गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां 
कारण शरीर की विशिष्टता भाव श्रद्धा
Read Scan Version
आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का उद्गम अन्तःकरण है जिसे कारण शरीर भी कहते हैं। प्राणिवर्ग में जो तुच्छ स्तर के हैं उनका केवल शरीर पौरुष ही गतिशील रहता है। जो इससे अधिक विकसित हैं, उनका मन मस्तिष्क और युद्ध कौशल भी एक सीमा तक करने लगता है। कारण शरीर समस्त प्राणि समुदाय में से किसी का भी विकसित और सक्षम नहीं होता है। अकेला मनुष्य ही है जो चेतना क्षेत्र में विकास कर सका है। उसकी अविकसित स्थिति तो नर वानरों जैसी ही होती है पर जैसे-जैसे मानवी गरिमा की परत खुलती जाती है वैसे-वैसे उसकी भाव सम्वेदना जगती हैं। आस्थाओं में परिपक्वता आती है और श्रद्धा का उत्कृष्टता अपनाने के लिए ऐसा प्रयास चल पड़ता है जिसे आत्मिक क्षेत्र का उत्कर्ष एवं अभ्युदय कहा जा सके। वस्तुतः मानवी गरिमा का शुभारम्भ यही से होता है।
आत्मिक प्रगति का एक ही लक्षण है आदर्श के मार्ग पर चलते को धकेल सकने जैसी क्षमता से सम्पन्न भाव संवेदना का उभरना। यह उभार वस्तुतः मानवी गरिमा का उन्नयन है। डण्ठल, डाली, पत्ते जब सभी परिपक्व हो जाते हैं तो कमल पुष्प खिलता है। पौधा जब तक कच्चा रहे तब तक उस पर सुविकसित पुष्प नहीं खिलता। इस प्रकार शरीरगत संयम और बुद्धिगत चिन्तन, मनन की परिपक्वता ही कारण शरीर को विकसित करती और मनुष्य को इस स्तर तक पहुँचाती है कि वह सद्भाव व श्रद्धा की सुविकसित स्थिति का अनुभव कर सके। यह श्रद्धा ही है जो अन्तराल को परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ सकने की परिस्थिति पैदा करती है।
श्रद्धा विहीन व्यक्ति साधनों से, दक्षताओं से, बौद्धिक विलक्षणताओं से कितना ही सुसज्जित क्यों न हो उसके अन्तराल की गहराई में श्रद्धा के अंकुर नहीं उग पाते। इस अभाव के रहते उस भूमिका में प्रवेश कर सकना बन नहीं पड़ता जिसे आदर्शवादी भाव संवेदना कहते हैं। जिसकी क्षमता से सद्गुणों के अनेकानेक पक्ष उभरते हैं। करुणा की अनुभूति होती है। आत्मीयता विकसित होती है। महानता का मार्ग अपनाने के लिए उमंग उठती है। मनुष्य में देवत्व का उदय यही है। उसे अपनी आत्मा में सबकी आत्मा और सबकी आत्मा में अपनी आत्मा परिलक्षित होती है। विराट् विश्व के कण कण में प्रभुसत्ता की उपस्थिति विद्यमान लगती है। जिस लोक में भगवान का निवास है वही स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग अपनी विकसित श्रद्धा ही अपने लिए अपना स्वतन्त्र स्वर्ग गढ़ लेती है। जिनमें निरन्तर निवास करते रहने और आनन्द से ओत प्रोत रहने का अवसर मिलता है। महामानवों जैसे स्वभाव संस्कार भी उसी स्थिति में विकसित होते हैं। ऐसे कृत्य भी उसी मनोदशा में करते बन पड़ते हैं, जिन्हें मनीषियों और तपस्वियों के जीवन में ही क्रियान्वित होते देखा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलने से जो अद्भुत अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है उसी के आधार पर देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि स्तर कीर देवात्माऐं अपनी स्थिति को असामान्य बनाती हैं। उनके क्रिया कलाप सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक उच्चस्तरीय होते हैं। वे सामान्य कार्य कलेवर में रहते तो हैं पर उनका दिशा निर्धारण, लक्ष्य संकल्प कुछ विशेष स्तर का ही होता है। स्थिति में इतना अन्तर आ जाता है कि गीता के अनुसार जब दुनिया सोती है तो योगी जागता है और जब योगी जागता है तब दुनिया सोती है। दोनों की स्थिति में रात दिन जैसा अन्तर होता है। संसारी लोग जहाँ स्वार्थ के लिए ही निरन्तर मरते खपते रहते हैं वहाँ श्रद्धावान् परमार्थ को लक्ष्य रखता है। उसे कर सकने के लिए अपनी अन्त: स्थिति को कषाय कल्मषों से विरत करते रहने में लगा रहता है। सांसारिक लोगों का लक्ष्य जहाँ संकीर्ण स्वार्थ परता की पूर्ति का होता है वहीं अध्यात्मवादी परमार्थ संचय के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं। एक जहाँ साधन सम्पदा से लदने के लिए उचित अनुचित का विचार तक छोड़ देता है वहाँ श्रद्धावान् न्यूनतम निर्वाह में काम चलाना और क्षमताओं का अपनी तथा दूसरों की संस्कृतियों को समुन्नत करने में नियोजित किए रहता है। दोनों के लक्ष्य और प्रयास में यह स्पष्ट अन्तर सहज ही जाना जा सकता है।
स्वार्थी लोग और अहंकार में डूबे पाए जाते हैं जबकि परमार्थी को सत्प्रवृत्तियों को बोने उगाने बढ़ाने से ही फुरसत नहीं मिलती। इसी को मनुष्य और देवता के बीच पाया जाने वाला अन्तर समझा जा सकता है। उपर्युक्त अन्तर के अनुरूप परिस्थितियाँ भी दोनों की अलग अलग होती हैं। एक की स्वार्थ साधन में व्यस्तता रहती है तो दूसरे की उत्कृष्टता के चरम शिखर पर जा पहुँचने की ललक लगी रहती है।
एक ही जंक्शन पर खड़ी दो रेल गाड़ियाँ दो विभिन्न दिशाओं के लिए छूटती हैं तो कुछ ही समय में दोनों के बीच भारी फासला पड़ जाता है। यही बात अनास्थावानों के बीच आस्थावानों के और भी होती है। एक नर पशु की तरह क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति में कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता है और बदले में अशान्ति, ईर्ष्या, दुर्व्यसन, भय, आतंक, अपमान में डूबा रहकर अपनी मनः स्थिति और परिस्थिति को उद्विग्नता की आग में जलाता रहता है। वहाँ दूसरा कल्पवृक्ष की तरह फलता फूलता और अपनी छाया में असंख्यों को सुख शान्ति भरा आनन्द अनुदान प्रदान करता रहता है। यह अन्तर श्रद्धा के भाव स्थायी अभाव के ऊपर ही निर्भर रहता है।
गीता के अनुसार सद्ज्ञान मात्र श्रद्धा के माध्यम से मिलता है। श्रद्धा ही विवेक की आँखें खोलती है। ऐसे दृष्टिवान को यथार्थता का बोध होता है। आत्म ज्ञान का दिव्य अनुदान मिलता है। अज्ञान का पर्दा हटने पर न दोष रहते हैं न दुर्गुण। न शोक रहता है और न सन्ताप। जिसने अपना कल्याण कर लिया वही दूसरे अन्य असंख्यों का कल्याण कर सकने में भी समर्थ है।
श्रद्धा प्रभाव और प्रताप सुविकसित व्यक्तित्व में ही परिलक्षित होता है। यहाँ प्रतिभा के रूप में वह गरिमा के रूप में प्रकट होता है। गाँधी जी चर्म चक्षुओं से देखने पर शरीर की दृष्टि से चकाचौंध उत्पन्न करने वाली प्रतिभा के धनी नहीं थें। फिर भी उनकी महानता हर गतिविधि से, हर उच्चारित शब्द से अपनी गरिमा का परिचय देती थी। श्रद्धावानों का व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्र में प्राय: इसी स्तर का हो जाता है। आन्तरिक उल्लास की अजस्र अनुभूति होने के अतिरिक्त उन्हें लोक सम्मान की जन सहयोग की भी कमी नहीं रहती। श्रद्धा अपने आप में परमात्म सत्ता का प्रत्यक्ष अनुदान है। वह जिसने अर्जित कर लिया समझना चाहिए कि उसने जीवन के सर्वांगीण सफलता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पशु और मनुष्य का अन्तर श्रद्धा के आधार पर ही आरम्भ होता है। अश्रद्धा को प्रत्यक्षवादी मन: स्थिति में किसी भी आदर्श का महत्त्व नहीं समझा जा सकता। परमार्थ की ओर एक कदम नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष स्वार्थ ही सब कुछ समझा जा सकता है। कोई किसी की परवाह क्यों करे ? अपनी विलासिता, लिप्सा, लालसा और महत्त्वाकाँक्षा पर कोई अंकुश क्यों लगाए ? स्वेच्छाचार बरतकर गर्व करने का अवसर क्यों खोए ? इस नियन्त्रण में तो अपने को रोकना प्रतिबन्धित ही करना पड़ेगा और दूसरों को लाभ देने की बात में अपने लिए तो घाटा ही है। आक्रमण से अनाचार से यदि लाभ उठाया जा सकता है तो दया धर्म के कारण असाधारण लाभ उठाने से क्यों चूका जाय ? उत्पीड़न, शोषण, छल, प्रपंच आदि पर अंकुश क्यों लगाया जाय ? इन सभी प्रसंगों में अनास्थावादी बुद्धि का यही निर्णय हो सकता है कि जिनमें स्वार्थ सधता हो वही किया जाय ? इस कारण दूसरों को क्या हानि होती है इसका विचार न किया जाय। ऐसी मन: स्थिति में पुण्य परमार्थ की बात सोचते भी नहीं बन पड़ती। क्योंकि उन सब में अर्थ प्रधान दृष्टि अपना अहित होने की बात ही सोचेगी। श्रद्धा ही है जो मनुष्य को विराट के साथ, आदर्शों के साथ, मानवी गरिमा के साथ जोड़ती है। जिसने उसे जिस रूप में पाया वह उसी गति से उत्कृष्टता को आध्यात्मिकता की दिशा में चल पड़ने के लिए तत्पर हुआ समझना चाहिए।
श्रद्धा और अन्ध श्रद्धा में जमीन आसमान जितना अन्तर है। अन्ध श्रद्धा पर अविवेक छाया रहता है। परम्परा का निर्वाह ही सब कुछ लगता है। उसमें उचित अनुचित का विश्लेषण करने का भी समय नहीं रहता। अनेकानेक कुरीतियां इस अन्ध श्रद्धा के आधार पर ही पनपी और पररिपक्व हुई हैं। इसी के सहारे घूर्तों ने मनगढंत संरचनाऐं रच कर मूर्खों को अपने चंगुल में फँसाया है। अन्ध श्रद्धा के साथ ही जो श्रद्धा शब्द लगा है और अपना कुप्रयोजन सिद्ध करने वाले उस अन्ध श्रद्धा की भी यथार्थता जैसी व्याख्या कर देते हैं पर वस्तुतः बात वैसी है नहीं। दोनों के बीच मृत और जीवित जैसा अन्तर है।
यों देवताओं के प्रति धर्म सम्प्रदायों के प्रति भी मान्यताओं का आग्रह रखा जाता है। पर वस्तुतः श्रद्धा भाव संवेदनाओं की उत्कृष्टता के साथ ही जुड़ी होती है। उसमें अन्तःकरण का ऐसा उल्लास जुड़ा होता है जिसकी प्रेरणा से हृदयता, सद्भावना और शालीनता को क्रियान्वित करने के लिए असाधारण उत्साह उभरे। कष्ट सहकर भी आदर्शों को अपनाए रहने की सतत् प्रेरणा मिले।
भावुकता और भावसंवेदना में अन्तर है। भावुकता एक आवेश है जब कि संवेदना अन्तःकरण का परिष्कृत स्तर। उसमें संकीर्ण स्वार्थ परता का लेश मात्र भी अंश नहीं होता। जो कुछ सोचते बन पड़ता है और क्रिया रूप में अपनाया जाता है उसमें आत्मीयता का गहरा पुट होता है। श्रद्धा इसी स्थिति की अभिव्यक्ति है। उसमें अपनी श्रेष्ठतम चेतना का अंश निचोड़ा जाता है और उसे निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए अर्पित किया जाता है। इसे कारण शरीर से उभरा हुआ वरदान भी कह सकते हैं।
आत्मिक प्रगति का एक ही लक्षण है आदर्श के मार्ग पर चलते को धकेल सकने जैसी क्षमता से सम्पन्न भाव संवेदना का उभरना। यह उभार वस्तुतः मानवी गरिमा का उन्नयन है। डण्ठल, डाली, पत्ते जब सभी परिपक्व हो जाते हैं तो कमल पुष्प खिलता है। पौधा जब तक कच्चा रहे तब तक उस पर सुविकसित पुष्प नहीं खिलता। इस प्रकार शरीरगत संयम और बुद्धिगत चिन्तन, मनन की परिपक्वता ही कारण शरीर को विकसित करती और मनुष्य को इस स्तर तक पहुँचाती है कि वह सद्भाव व श्रद्धा की सुविकसित स्थिति का अनुभव कर सके। यह श्रद्धा ही है जो अन्तराल को परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ सकने की परिस्थिति पैदा करती है।
श्रद्धा विहीन व्यक्ति साधनों से, दक्षताओं से, बौद्धिक विलक्षणताओं से कितना ही सुसज्जित क्यों न हो उसके अन्तराल की गहराई में श्रद्धा के अंकुर नहीं उग पाते। इस अभाव के रहते उस भूमिका में प्रवेश कर सकना बन नहीं पड़ता जिसे आदर्शवादी भाव संवेदना कहते हैं। जिसकी क्षमता से सद्गुणों के अनेकानेक पक्ष उभरते हैं। करुणा की अनुभूति होती है। आत्मीयता विकसित होती है। महानता का मार्ग अपनाने के लिए उमंग उठती है। मनुष्य में देवत्व का उदय यही है। उसे अपनी आत्मा में सबकी आत्मा और सबकी आत्मा में अपनी आत्मा परिलक्षित होती है। विराट् विश्व के कण कण में प्रभुसत्ता की उपस्थिति विद्यमान लगती है। जिस लोक में भगवान का निवास है वही स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग अपनी विकसित श्रद्धा ही अपने लिए अपना स्वतन्त्र स्वर्ग गढ़ लेती है। जिनमें निरन्तर निवास करते रहने और आनन्द से ओत प्रोत रहने का अवसर मिलता है। महामानवों जैसे स्वभाव संस्कार भी उसी स्थिति में विकसित होते हैं। ऐसे कृत्य भी उसी मनोदशा में करते बन पड़ते हैं, जिन्हें मनीषियों और तपस्वियों के जीवन में ही क्रियान्वित होते देखा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलने से जो अद्भुत अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है उसी के आधार पर देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि स्तर कीर देवात्माऐं अपनी स्थिति को असामान्य बनाती हैं। उनके क्रिया कलाप सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक उच्चस्तरीय होते हैं। वे सामान्य कार्य कलेवर में रहते तो हैं पर उनका दिशा निर्धारण, लक्ष्य संकल्प कुछ विशेष स्तर का ही होता है। स्थिति में इतना अन्तर आ जाता है कि गीता के अनुसार जब दुनिया सोती है तो योगी जागता है और जब योगी जागता है तब दुनिया सोती है। दोनों की स्थिति में रात दिन जैसा अन्तर होता है। संसारी लोग जहाँ स्वार्थ के लिए ही निरन्तर मरते खपते रहते हैं वहाँ श्रद्धावान् परमार्थ को लक्ष्य रखता है। उसे कर सकने के लिए अपनी अन्त: स्थिति को कषाय कल्मषों से विरत करते रहने में लगा रहता है। सांसारिक लोगों का लक्ष्य जहाँ संकीर्ण स्वार्थ परता की पूर्ति का होता है वहीं अध्यात्मवादी परमार्थ संचय के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं। एक जहाँ साधन सम्पदा से लदने के लिए उचित अनुचित का विचार तक छोड़ देता है वहाँ श्रद्धावान् न्यूनतम निर्वाह में काम चलाना और क्षमताओं का अपनी तथा दूसरों की संस्कृतियों को समुन्नत करने में नियोजित किए रहता है। दोनों के लक्ष्य और प्रयास में यह स्पष्ट अन्तर सहज ही जाना जा सकता है।
स्वार्थी लोग और अहंकार में डूबे पाए जाते हैं जबकि परमार्थी को सत्प्रवृत्तियों को बोने उगाने बढ़ाने से ही फुरसत नहीं मिलती। इसी को मनुष्य और देवता के बीच पाया जाने वाला अन्तर समझा जा सकता है। उपर्युक्त अन्तर के अनुरूप परिस्थितियाँ भी दोनों की अलग अलग होती हैं। एक की स्वार्थ साधन में व्यस्तता रहती है तो दूसरे की उत्कृष्टता के चरम शिखर पर जा पहुँचने की ललक लगी रहती है।
एक ही जंक्शन पर खड़ी दो रेल गाड़ियाँ दो विभिन्न दिशाओं के लिए छूटती हैं तो कुछ ही समय में दोनों के बीच भारी फासला पड़ जाता है। यही बात अनास्थावानों के बीच आस्थावानों के और भी होती है। एक नर पशु की तरह क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति में कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता है और बदले में अशान्ति, ईर्ष्या, दुर्व्यसन, भय, आतंक, अपमान में डूबा रहकर अपनी मनः स्थिति और परिस्थिति को उद्विग्नता की आग में जलाता रहता है। वहाँ दूसरा कल्पवृक्ष की तरह फलता फूलता और अपनी छाया में असंख्यों को सुख शान्ति भरा आनन्द अनुदान प्रदान करता रहता है। यह अन्तर श्रद्धा के भाव स्थायी अभाव के ऊपर ही निर्भर रहता है।
गीता के अनुसार सद्ज्ञान मात्र श्रद्धा के माध्यम से मिलता है। श्रद्धा ही विवेक की आँखें खोलती है। ऐसे दृष्टिवान को यथार्थता का बोध होता है। आत्म ज्ञान का दिव्य अनुदान मिलता है। अज्ञान का पर्दा हटने पर न दोष रहते हैं न दुर्गुण। न शोक रहता है और न सन्ताप। जिसने अपना कल्याण कर लिया वही दूसरे अन्य असंख्यों का कल्याण कर सकने में भी समर्थ है।
श्रद्धा प्रभाव और प्रताप सुविकसित व्यक्तित्व में ही परिलक्षित होता है। यहाँ प्रतिभा के रूप में वह गरिमा के रूप में प्रकट होता है। गाँधी जी चर्म चक्षुओं से देखने पर शरीर की दृष्टि से चकाचौंध उत्पन्न करने वाली प्रतिभा के धनी नहीं थें। फिर भी उनकी महानता हर गतिविधि से, हर उच्चारित शब्द से अपनी गरिमा का परिचय देती थी। श्रद्धावानों का व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्र में प्राय: इसी स्तर का हो जाता है। आन्तरिक उल्लास की अजस्र अनुभूति होने के अतिरिक्त उन्हें लोक सम्मान की जन सहयोग की भी कमी नहीं रहती। श्रद्धा अपने आप में परमात्म सत्ता का प्रत्यक्ष अनुदान है। वह जिसने अर्जित कर लिया समझना चाहिए कि उसने जीवन के सर्वांगीण सफलता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पशु और मनुष्य का अन्तर श्रद्धा के आधार पर ही आरम्भ होता है। अश्रद्धा को प्रत्यक्षवादी मन: स्थिति में किसी भी आदर्श का महत्त्व नहीं समझा जा सकता। परमार्थ की ओर एक कदम नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष स्वार्थ ही सब कुछ समझा जा सकता है। कोई किसी की परवाह क्यों करे ? अपनी विलासिता, लिप्सा, लालसा और महत्त्वाकाँक्षा पर कोई अंकुश क्यों लगाए ? स्वेच्छाचार बरतकर गर्व करने का अवसर क्यों खोए ? इस नियन्त्रण में तो अपने को रोकना प्रतिबन्धित ही करना पड़ेगा और दूसरों को लाभ देने की बात में अपने लिए तो घाटा ही है। आक्रमण से अनाचार से यदि लाभ उठाया जा सकता है तो दया धर्म के कारण असाधारण लाभ उठाने से क्यों चूका जाय ? उत्पीड़न, शोषण, छल, प्रपंच आदि पर अंकुश क्यों लगाया जाय ? इन सभी प्रसंगों में अनास्थावादी बुद्धि का यही निर्णय हो सकता है कि जिनमें स्वार्थ सधता हो वही किया जाय ? इस कारण दूसरों को क्या हानि होती है इसका विचार न किया जाय। ऐसी मन: स्थिति में पुण्य परमार्थ की बात सोचते भी नहीं बन पड़ती। क्योंकि उन सब में अर्थ प्रधान दृष्टि अपना अहित होने की बात ही सोचेगी। श्रद्धा ही है जो मनुष्य को विराट के साथ, आदर्शों के साथ, मानवी गरिमा के साथ जोड़ती है। जिसने उसे जिस रूप में पाया वह उसी गति से उत्कृष्टता को आध्यात्मिकता की दिशा में चल पड़ने के लिए तत्पर हुआ समझना चाहिए।
श्रद्धा और अन्ध श्रद्धा में जमीन आसमान जितना अन्तर है। अन्ध श्रद्धा पर अविवेक छाया रहता है। परम्परा का निर्वाह ही सब कुछ लगता है। उसमें उचित अनुचित का विश्लेषण करने का भी समय नहीं रहता। अनेकानेक कुरीतियां इस अन्ध श्रद्धा के आधार पर ही पनपी और पररिपक्व हुई हैं। इसी के सहारे घूर्तों ने मनगढंत संरचनाऐं रच कर मूर्खों को अपने चंगुल में फँसाया है। अन्ध श्रद्धा के साथ ही जो श्रद्धा शब्द लगा है और अपना कुप्रयोजन सिद्ध करने वाले उस अन्ध श्रद्धा की भी यथार्थता जैसी व्याख्या कर देते हैं पर वस्तुतः बात वैसी है नहीं। दोनों के बीच मृत और जीवित जैसा अन्तर है।
यों देवताओं के प्रति धर्म सम्प्रदायों के प्रति भी मान्यताओं का आग्रह रखा जाता है। पर वस्तुतः श्रद्धा भाव संवेदनाओं की उत्कृष्टता के साथ ही जुड़ी होती है। उसमें अन्तःकरण का ऐसा उल्लास जुड़ा होता है जिसकी प्रेरणा से हृदयता, सद्भावना और शालीनता को क्रियान्वित करने के लिए असाधारण उत्साह उभरे। कष्ट सहकर भी आदर्शों को अपनाए रहने की सतत् प्रेरणा मिले।
भावुकता और भावसंवेदना में अन्तर है। भावुकता एक आवेश है जब कि संवेदना अन्तःकरण का परिष्कृत स्तर। उसमें संकीर्ण स्वार्थ परता का लेश मात्र भी अंश नहीं होता। जो कुछ सोचते बन पड़ता है और क्रिया रूप में अपनाया जाता है उसमें आत्मीयता का गहरा पुट होता है। श्रद्धा इसी स्थिति की अभिव्यक्ति है। उसमें अपनी श्रेष्ठतम चेतना का अंश निचोड़ा जाता है और उसे निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए अर्पित किया जाता है। इसे कारण शरीर से उभरा हुआ वरदान भी कह सकते हैं।
Versions
-
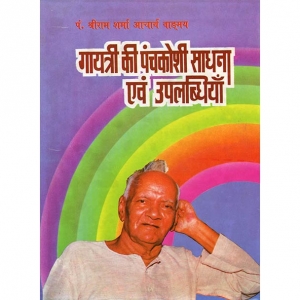
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-1Scan Book Version
-
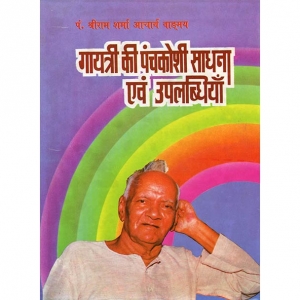
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियाँ भाग-2Scan Book Version
-
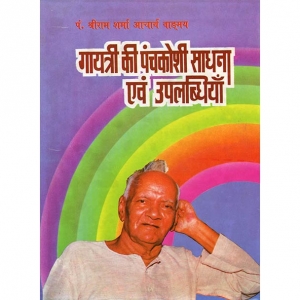
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-3Scan Book Version
-
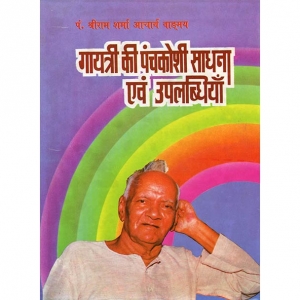
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-4Scan Book Version
-
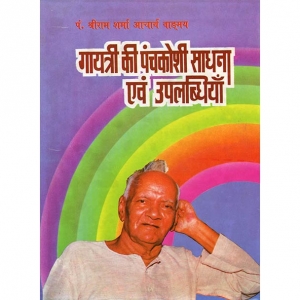
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-5Scan Book Version
-
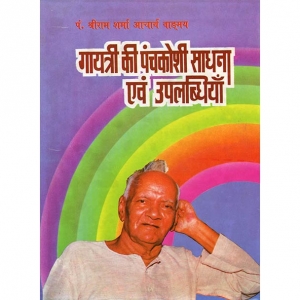
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-6Scan Book Version
-
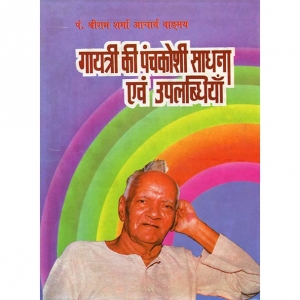
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियांText Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री साधना के दो स्तर
- उच्चस्तरीय साधना और उसकी सिद्धि
- उच्चस्तरीय साधना का तत्त्वज्ञान
- गायत्री के पाँच मुख
- देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य
- गायत्री माता की दस भुजायें और उनका रहस्य
- प्रतीक का निष्कर्ष
- गायत्री का भावनात्मक एवं वैज्ञानिक महत्व
- गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोश
- अनन्त आनन्द की साधना
- पाँच कोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया
- पाँच कोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि
- चेतना के पाँच आयाम पंच कोश उपासना
- सूक्ष्म शरीर के पाँच कोश एवं उनका वैज्ञानिक विवेचन
- मानवी काया की चेतनसत्ता का वैज्ञानिक विवेचन वैज्ञानिक अध्यात्मवाद
- पंच कोश और उनका अनावरण
- जीवात्मा के तीन शरीर और उनकी साधना
- तीन शरीर और उनका कार्य क्षेत्र
- कायसत्ता के तीन कलेवर एवं उनका अनावरण
- चारों ओर बिखरा सूक्ष्म का सिराजा
- अन्तराल में समाई दिव्य शक्तियाँ सिद्धियाँ
- मनुष्य देह में भरा विलक्षण विराट
- स्थूल शरीर का परिष्कार कर्मयोग से
- सूक्ष्म शरीर की महती सामर्थ्य
- सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा और उसकी विशिष्ट क्षमता
- प्रमाणित तो होता है, सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व
- सूक्ष्म शरीर के अविज्ञात क्रिया कलाप
- सूक्ष्मीकरण की अनेक गुनी सामर्थ्य
- सूक्ष्म शरीर का दिव्यीकरण
- सूक्ष्म शरीर के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि
- सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष ज्ञानयोग से
- भाव संवेदनाओं का भाण्डागार: कारण शरीर
- कारण शरीर देव शरीर
- कारण शरीर की विशिष्टता भाव श्रद्धा
- कारण शरीर का उत्कर्ष भक्तियोग से
- स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म और कारण
- योग साधना की तीन धाराएँ
- त्रिविध शरीरों की समन्वित साधना
- हमारा अद्भुत विलक्षण अन्नमय कोश
- जीव सत्ता की प्रचण्ड शक्ति सामर्थ्य
- अन्नमय कोश और चमत्कारी हार्मोन ग्रन्थियाँ
- हमारे शरीर के रहस्यमय घटक जीन्स
- अन्नमय कोश का परिष्कार और प्रतिफल
- अन्नमय कोश और उसका अनावरण
- अन्नमय कोश की जाग्रति, आहार शुद्धि से
- आहार के त्रिविध स्तर, त्रिविध प्रयोजन
- आहार, संयम और अन्नमय कोश का जागरण
- आहार विहार से जुड़ा है मन
- आहार और उसकी शुद्धि
- आहार शुद्धौः सत्व शुद्धौः
- अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति
- उपवास का आध्यात्मिक महत्त्व
- उपवास से सूक्ष्म शक्ति की अभिवृद्धि
- उपवास से उपत्यिकाओं का शोधन
- उपवास के प्रकार
- उच्चस्तरीय गायत्री साधना और आसन
- आसनों का काय विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रभाव
- आसनों के प्रकार
- सूर्य नमस्कार की विधि
- पंच तत्वों की साधना तत्व साधना एक महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म विज्ञान
- तत्व शुद्धि
- तपश्चर्या से आत्मबल की उपलब्धि
- आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है
- तपस्या का प्रचण्ड प्रताप
- तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का उद्भव
- ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- प्राणमय कोश और उसका विकास
- प्राण शक्ति का स्वरूप और अभिवर्धन
- प्राणमय कोश में सन्निहित प्रचण्ड जीवनी शक्ति-प्राण
- प्राणायाम और प्राणशक्ति
- प्राणायाम से प्राणमय कोश का परिष्कार
- प्राणमय-कोश की साधना
- प्राणाकर्षण की क्रियायें
- पाँच प्राणों की साधना-पाँच कोशों की सिद्धि
- पाँच प्राण-पाँच उपप्राणों की अद्भुत शक्ति धाराएँ
- मूल बंध, उड्डियान बंध और जालंधर बंध का रहस्य
- मुद्रा उपचार
- नौ प्राणायाम
- मनोमय कोश का अनावरण
- मनोमय कोश का विकास परिष्कार
- मनोमय कोश की साधना से सर्वार्थ सिद्धि
- मन और उसका निग्रह
- ध्यान
- त्राटक
- त्राटक-साधन से एकाग्रता शक्ति का अभिवर्द्धन
- मनोमय कोश और आज्ञा चक्र
- त्राटक साधना से दिव्य दृष्टि की जागृति
- जप साधना
- पंच तन्मात्राओं की साधनाएँ तथा सिद्धियाँ
- पंच तन्मात्राओं का पंच ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्ध
- शब्द साधना
- रूप साधना
- छाया पुरुष- हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर
- रस साधना
- गन्ध साधना
- स्पर्श- साधना
- विज्ञानमय कोश का जागरण
- विज्ञानमय कोश-सूक्ष्म सिद्धियों का केन्द्र
- विज्ञानमय कोश का केन्द्र संस्थान हृदयचक्र
- विज्ञानमय कोश और जीवन साधना
- विज्ञानमय कोश का जागरण
- सोऽहम् साधना
- आत्मानुभूति-योग
- आत्मदर्शन की समर्थ साधना
- आत्म- चिन्तन की साधना
- दूसरी साधना
- स्वर योग
- आत्मानुभूति-योग
- स्वर बदलना
- स्वर-संयम से दीर्घ जीवन
- विज्ञानमय-कोश की वायु साधना
- त्रिविधि बंधन और उनसे मुक्ति
- ग्रन्थि- बेध
- आनन्दमय कोश का अनावरण
- आनन्दमय कोश-शिव शक्ति का संगम
- २७ समाधियों में सर्वोत्तम सहज समाधि
- आनन्दमय कोश अनावरण
- नाद साधना
- नाद साधना का क्रमिक अभ्यास
- आनन्दमय कोश की तीन उपलब्धियाँ समाधि, स्वर्ग और मुक्ति
- बिन्दु साधना
- नादयोग- दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान
- बिन्दुभेद की साधना-विधि
- कला- साधना
- पाँचकलाओं द्वारा तात्विक साधना
- तुरीय अवस्था

