गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां 
सोऽहम् साधना
Read Scan Version
आत्मा के सूक्ष्म अन्तराल में अपने आप के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है ताकि बुद्धि भ्रमित न हो और अपने स्वरूप को न भूले। थोड़ा-सा ध्यान देने पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उस ध्वनि पर निरन्तर ध्यान दिया जाय तो उस घोषणा के करने वाले अमृत भण्डार आत्मा तक भी पहुँचा जा सकता है।
जब एक साँस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ-साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द “सो ो ो ो ो '' जैसा होता है। जितनी देर साँस भीतर ठहरती है अर्थात् स्वाभाविक कुंभक होता है उतनी देर आधे 'ऽऽऽऽ' की सी विराम ध्वनि होती है और जब साँस बाहर निकलती है तो '' हं...... '' जैसी ध्वनि निकलती है। इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केन्द्रित करने से, अजपा-जाप की 'सोऽहम् '' साधना होने लगती है।
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्यकर्म से निबट कर पूर्व को मुख करके किसी शान्त स्थान पर बैठिये। मेरुदण्ड सीधा रहे। दोनों हाथों को समेट कर गोदी में रख लीजिए नेत्र बन्द कर रखिये। जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे, तो सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय को सजग करके ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ-साथ ‘सो' की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके 'अ ' और वायु निकलते समय ‘ हं ' की ध्वनि पर ध्यान केन्द्रित कीजिये। साथ ही हृदय स्थिति सूर्य-चक्र के प्रकाश बिन्दु में आत्मा के तेजोमय स्फुल्लिंग की श्रद्धा कीजिए। जब साँस भीतर जा रही हो और 'सो' की ध्वनि हो रही हो तब अनुभव कीजिए कि यह तेज बिन्दु परमात्मा का प्रकाश है 'स' अर्थात् परमात्मा 'ऽहम् '' अर्थात्- मैं। जब वायु बाहर निकलने और ‘हं’ की ध्वनि हो तब उसी प्रकाश बिन्दु में भावना कीजिए कि यह मैं हूँ।''
इस तरह श्वाँस लेते समय 'सो' ध्वनि का और छोड़ते समय 'हम' ध्यान के प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अन्त: भूमिका मे अनुभव करना, यही है संक्षेप में 'सोऽहम्' साधना।
वायु जब छोटे छिद्र में होकर वेगपूर्वक निकलती है तो के कारण ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है, बाँसुरी से स्वर लहरी निकलने का यही आधार है। जंगलों में जहाँ बाँस बहुत उगे होते हैं वहाँ अक्सर बाँसुरी जैसी ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं। कारण कि बाँसों में कहीं- कहीं कीड़े छेद कर देते हैं और उस छेदों से जब हवा वेगपूर्वक टकराती है तो उसमें उत्पन्न स्वर प्रवाह सुनने को मिलता है। वृक्षों से टकराकर जब द्रुतगति से हवा चलती है तब सन-सनाहट सुनाई पड़ती है, यह वायु के घर्षण की ही प्रतिक्रिया है।
नासिका छिद्र भी बाँसुरी के छिद्रों की तरह हैं, उनकी सीमित परिधि में होकर जब वायु भीतर प्रवेश करेगी तो वहाँ स्वभावतः ध्वनि उत्पन्न होगी। साधारण श्वाँस- प्रश्वाँस के समय भी वह उत्पन्न होता है, पर इतनी धीमी रहती है कि कानों के छिद्र उन्हें सरलतापूर्वक नहीं सुन सकते। प्राणयोग की साधना में गहरे श्वाँसोच्छ्वास लेने पड़ते हैं। प्राणायाम का मूल स्वरूप ही यह है कि श्वाँस जितनी अधिक गहरी, जितनी मन्दगति से ली जा सके लेनी चाहिए और फिर कुछ समय भीतर रोककर धीरे-धीरे उस वायु को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए। गहरी और पूरी साँस लेने में स्वभावतः नासिका छिद्रों से टकराकर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी अधिक तीव्र हो जाता है। इतने पर भी वह ऐसा नहीं बन पाता कि खुले कानों से उसे सुना जा सके। कर्णेन्द्रियों की सूक्ष्म चेतना में ही उसे अनुभव किया जा सकता है।
चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस स्तर की बनाना चाहिए कि उसे श्वाँस लेते समय 'सो' शब्द के ध्वनि प्रवाह की मन्द अनुभूति होने लगे। उसी प्रकार जब साँस छोड़ना पड़े तो यह मान्यता परिपक्व करनी चाहिए कि ‘हम् 'ध्वनि प्रवाह विनिर्मित हो रहा है। आरम्भ में कुछ समय यह अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं होती किन्तु क्रम और प्रयास जारी रखने पर कुछ ही समय उपरान्त इस प्रकार का ध्वनि प्रवाह अनुभव में आने लगता है और उसे सुनने में न केवल चित्त ही एकाग्र होता है, वरन् आनन्द का अनुभव होता है।
'सो' का तात्पर्य परमात्मा और हम् का जीव चेतना समझा जाना चाहिए। निखिल विश्व ब्रह्माण्ड में संव्याप्त महाप्राण नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अंग-प्रत्यंग में जीवकोश तथा नाड़ी तन्त्र में प्रवेश करके उसको अपने सम्पर्क संसर्ग का लाभ प्रदान करता है। यह अनुभूति ‘सो' शब्द ध्वनि के साथ अनुभूति भूमिका में उतरनी चाहिए और ‘हम' शब्द के साथ जीव भाव द्वारा इस काय-कलेवर पर से अपना कब्जा छोड़कर चले जाने की मान्यता प्रगाढ़ की जानी चाहिए।
प्रकारान्तर से परमात्म सत्ता का अपने शरीर और मनःक्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाने की ही यह धारणा है। जीव भाव अर्थात् स्वार्थवादी संकीर्णता काम, क्रोध, लोभ, मोह, भरी मद मत्सरता अपने को शरीर या मन के रूप में अनुभव करते रहने वाली आत्मा की दिग्भ्रान्त स्थिति का नाम ही जीव भूमिका है। इस भ्रम- जंजाल भरे जीव- भाव को हटा दिया जाये तो फिर अपना विशुद्ध अस्तित्व ईश्वर के अविनाशी अंश आत्मा के रूप में ही शेष रह जाता है। काय कलेवर के कण-कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना और जीव धारण की बेदखली यही है सोऽहम् साधना का तत्वज्ञान। श्वाँस-प्रश्वाँस क्रिया के माध्यम से सो और हम ध्वनि के सहारे इसी भाव-चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है। अब शरीर और मन पर से लोभ-मोह का, वासना-तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है और उसके स्थान पर उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व के रूप में ब्रह्यसता की स्थापना हो रही है। शासन परिवर्तन जैसी यह भाव भूमिका है, जिसमें अनाधिकारी-अनाचारी शासनसत्ता का तख्ता उलटकर उस स्थान पर सत्य, न्याय और प्रेम के संविधान वाली धर्मसत्ता का राज्याभिषेक किया जाता है। सोऽहम् साधना इसी अनुभूति स्तर को क्रमश प्रगाढ़ करती चली जाती है, और अन्तःकरण यह अनुभव करने लगता है कि अब उस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा, उसका समग्र संचालन देव सत्ता द्वारा किया जा सकता है।
श्वाँस ध्वनि ग्रहण करते समय ‘सो' और निकालते समय 'हम' की धारणा में लगना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि इन शब्दों के आरम्भ में अति मन्द स्तर की होने वाली अनुभूति में क्रमश: प्रखरता आती चली जाये। चिंतन का स्वरूप यह होना चाहिए कि साँस में घुले हुए भगवान अपनी समस्त विभूतियों और विशेषताओं के साथ काय-कलेवर में भीतर प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश मात्र आवागमन नहीं है वरन् प्रत्येक अवयव पर सघन आधिपत्य बन रहा है। एक-एक करके शरीर के भीतरी प्रमुख अंगों के चित्र की कल्पना करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि उसमें भगवान की सत्ता चिरस्थाई रूप से समाविष्ट हो गई। हृदय फुफ्फुस आमाशय, आँतें, गुर्दे, जिगर, तिल्ली आदि में भगवान का प्रवेश हो गया। रक्त के साथ प्रत्येक नस-नाड़ी और कोशिकाओं पर भगवान ने अपना शासन स्थापित कर लिया। बाह्य अंगों ने, पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच ज्ञानेन्द्रियों, ने भगवान के अनुशासन में रहना और उनका निर्देश पालन करना स्वीकार कर लिया। जीभ वही बोलेगी जो ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक हो। देखना, सुनना, बोलना, चलना आदि इन्द्रियजन्य गतिविधियाँ दिव्य निर्देशों का ही अनुगमन करेंगी। ज्ञानेन्द्रिय का उपयोग वासना के लिए नहीं मात्र ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए अनिवार्य आवश्यकता का धर्म संकट सामने आ खड़ा होने पर ही किया जायेगा। हाथ-पाँव मानवोचित कर्तव्य पालन के अतिरिक्त ऐसा कुछ न करेंगे जो ईश्वरीय सत्ता को कलंकित करता हो। मस्तिष्क ऐसा कुछ न सोचेगा जिसे उच्च आदर्शों के प्रतिकूल ठहराया जा सके। बुद्धि कोई अनुचित न्याय विरुद्ध एवं अदूरदर्शी-अविवेक भरा निर्णय न करेगी। चित्त में अवांछनीय एवं निकृष्ट स्तरीय आकांक्षायें न जमने पायेंगी। अहंता का स्तर नर कीटक जैसा नर-नारायण जैसा होगा।
यही हैं वे भावनायें जो शरीर और मन पर भगवान का शासन स्थापित होने के तथ्य को यथार्थ सिद्ध कर सकती हैं। यह सब उथली कल्पनाओं की तरह मनोविनोद भर नहीं रह जाना चाहिए वरन् उसकी आस्था इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि इस भाव परिवर्तन को क्रिया रूप में परिणत हुए बिना चैन ही न पड़े। सार्थकता उन्हीं विचारों की है जो क्रिया रूप में परिणत होने की प्रखरता से भरे हों।सोऽहम् साधना के पूर्वार्द्ध में अपने काय-कलेवर पर श्वसन क्रिया के साथ प्रविष्ट हुए महाप्राण की, परब्रह्म की सत्ता स्थापना का इतना गहन चिंतन करना पड़ता है कि यह कल्पना स्तर की बात न रहकर एक व्यवहारिक यथार्थता के, प्रत्यक्ष तथ्य के रूप में प्रस्तुत- दृष्टिगोचर होने लगे।
इस साधना का उत्तरार्द्ध पाप निष्कासन का है। शरीर में से अवांछनीय इन्द्रिय लिप्साओं का, आलस्य- प्रमाद जैसी दृष्प्रवृतियों का, मन से लोभ-मोह जैसी तृष्णाओं का, अन्तःस्थल से जीवभावी अहन्ता का निवारण-निराकरण हो रहा है। ऐसी भावनाएँ अत्यन्त प्रगाढ़ होनी चाहिए। दुर्भावनाएँ और दुष्कृतियाँ, निकृष्टताएँ और दुष्टताएँ और हीनताएँ सभी निरस्त हो रही हैं, सभी पालयन कर रही हैं- यह तथ्य हर पड़ी सामने दीखना चाहिए। अनुपयुक्तताओं के निरस्त होने के उपरान्त जो हलकापन, जो सन्तोष, जो उल्लास स्वभावत: होता है और निरन्तर बना रहता है, उसी का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। तभी यह कहा जा सकेगा कि सोऽहम् साधना का उत्तरार्द्ध भी एक तथ्य बन गया।
सोऽहम् साधना के पूर्व भाग में श्वाँस लेते समय ‘सो' ध्वनि के साथ जीवन सत्ता पर उस परब्रह्म परमात्मा का शासन- आधिपत्य स्थापित होने की स्वीकृति है। उत्तरार्द्ध में 'हम' को, अहंता को विसर्जित करने का भाव है। साँस निकलने के साथ-साथ अहम् भाव का भी निष्कासन हुआ। अहंता ही लोभ और मोह की जननी है। शरीराभ्यास में जीव उसी की प्रबलता के कारण डूबता है। माया, अज्ञान, अन्धकार, बन्धन आदि की भ्रान्तियाँ एवं विपत्तियाँ इस अहंता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसे विसर्जित कर देने पर ही भगवान का अन्त:क्षेत्र में प्रवेश करना, निवास करना सम्भव होता है।
इस छोटे से मानवी अन्तःकरण में दो के निवास की गुंजायश नहीं पूरी तरह एक ही रह सकता है, दोनों रहे तो लड़ते-झगड़ते रहते हैं और अन्तर्द्वन्द की खींचतान चलती रहती है। भगवान को बहिष्कृत करके पूरी तरह 'अहमन्यता' को प्रबल बना लिया जाय तो मनुष्य दुष्ट- दुर्बुद्धि, क्रूरकर्मा, असुर बनता है। अपनी कामनाएँ, भौतिक महत्त्वाकाँक्षाएँ, ऐषणाएँ समाप्त करके ईश्वरीय निर्देशों पर चलने का संकल्प ही आत्म-समर्पण है। यही शरणागति है, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त होते ही मनुष्य में देवत्व का उदय होता है, तब ईश्वरीय अनुभूतियाँ चिंतन में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता भर देती है। ऐसे ही व्यक्ति महामानव, ऋषि, देवता एवं अवतार के नाम से पुकारे जाते हैं। ‘सो' में भगवान का शासन आत्मसत्ता पर स्थापित करने और हम' में अहंता का विसर्जन करने का भाव है। प्रकारान्तर से इसे महान् परिवर्तन का, आंतरिक कायाकल्प का बीजारोपण कह सकते हैं। सोऽहम् साधना का यही है भावनात्मक एवं व्यावहारिक स्वरूप।
सोऽहम् साधना में 'अ' की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। आरम्भ में उस हृदय-चक्र स्थिति बिन्दु को ‘सो' ध्वनि के समय ब्रह्म माना जाता है और पीछे उसी की 'हं' धारणा में जीव भावना हो जाती हैं। बस भाव परिवर्तन के लिए 'अ' का अवकाश काल रखा गया है इसी प्रकार जब 'हं' समाप्त हो जाय, वायु बाहर निकल जाय और नया वायु प्रवेश करे उस समय भी दीन-भाव हटाकर उस तेज बिन्दु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। वह दोनों ही अवकाश 'अऽऽ ऽ' के समान हैं, इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। शब्द तो सो'ऽहं' का ही होता है।
‘सो' ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है। 'ऽ' प्रकृति का प्रतिनिधि है। 'हं' जीव का प्रतीक हैं। ब्रह्म, प्रकृति और जीव का सम्मिलन इस अजपा-जाप में होता है। सोऽहम्- साधना में तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म-जागरण का स्वर्ण सुयोग एक साथ ही उपलब्ध होने लगता है।
सोहम्' साधना की उन्नति जैसे-जैसे होती जाती है वैसे ही वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता जाता है। आत्म-ज्ञान बढ़ता है और धीरे-धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चलती है। आगे चलकर साँस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय स्थित सूर्य-चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हैं। उस समय समाधि की सी अवस्था हो जाती है। हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है।
स्वामी विवेकानन्द ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिए ''आत्मानुभूति'' की विधि बताई है। उनके अमेरिकन शिष्य रामाचरक ने इस विधि को ‘मेण्टल डेवलपमेण्ट ' नामक पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखा है।
जब एक साँस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ-साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द “सो ो ो ो ो '' जैसा होता है। जितनी देर साँस भीतर ठहरती है अर्थात् स्वाभाविक कुंभक होता है उतनी देर आधे 'ऽऽऽऽ' की सी विराम ध्वनि होती है और जब साँस बाहर निकलती है तो '' हं...... '' जैसी ध्वनि निकलती है। इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केन्द्रित करने से, अजपा-जाप की 'सोऽहम् '' साधना होने लगती है।
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्यकर्म से निबट कर पूर्व को मुख करके किसी शान्त स्थान पर बैठिये। मेरुदण्ड सीधा रहे। दोनों हाथों को समेट कर गोदी में रख लीजिए नेत्र बन्द कर रखिये। जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे, तो सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय को सजग करके ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ-साथ ‘सो' की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके 'अ ' और वायु निकलते समय ‘ हं ' की ध्वनि पर ध्यान केन्द्रित कीजिये। साथ ही हृदय स्थिति सूर्य-चक्र के प्रकाश बिन्दु में आत्मा के तेजोमय स्फुल्लिंग की श्रद्धा कीजिए। जब साँस भीतर जा रही हो और 'सो' की ध्वनि हो रही हो तब अनुभव कीजिए कि यह तेज बिन्दु परमात्मा का प्रकाश है 'स' अर्थात् परमात्मा 'ऽहम् '' अर्थात्- मैं। जब वायु बाहर निकलने और ‘हं’ की ध्वनि हो तब उसी प्रकाश बिन्दु में भावना कीजिए कि यह मैं हूँ।''
इस तरह श्वाँस लेते समय 'सो' ध्वनि का और छोड़ते समय 'हम' ध्यान के प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अन्त: भूमिका मे अनुभव करना, यही है संक्षेप में 'सोऽहम्' साधना।
वायु जब छोटे छिद्र में होकर वेगपूर्वक निकलती है तो के कारण ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है, बाँसुरी से स्वर लहरी निकलने का यही आधार है। जंगलों में जहाँ बाँस बहुत उगे होते हैं वहाँ अक्सर बाँसुरी जैसी ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं। कारण कि बाँसों में कहीं- कहीं कीड़े छेद कर देते हैं और उस छेदों से जब हवा वेगपूर्वक टकराती है तो उसमें उत्पन्न स्वर प्रवाह सुनने को मिलता है। वृक्षों से टकराकर जब द्रुतगति से हवा चलती है तब सन-सनाहट सुनाई पड़ती है, यह वायु के घर्षण की ही प्रतिक्रिया है।
नासिका छिद्र भी बाँसुरी के छिद्रों की तरह हैं, उनकी सीमित परिधि में होकर जब वायु भीतर प्रवेश करेगी तो वहाँ स्वभावतः ध्वनि उत्पन्न होगी। साधारण श्वाँस- प्रश्वाँस के समय भी वह उत्पन्न होता है, पर इतनी धीमी रहती है कि कानों के छिद्र उन्हें सरलतापूर्वक नहीं सुन सकते। प्राणयोग की साधना में गहरे श्वाँसोच्छ्वास लेने पड़ते हैं। प्राणायाम का मूल स्वरूप ही यह है कि श्वाँस जितनी अधिक गहरी, जितनी मन्दगति से ली जा सके लेनी चाहिए और फिर कुछ समय भीतर रोककर धीरे-धीरे उस वायु को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए। गहरी और पूरी साँस लेने में स्वभावतः नासिका छिद्रों से टकराकर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी अधिक तीव्र हो जाता है। इतने पर भी वह ऐसा नहीं बन पाता कि खुले कानों से उसे सुना जा सके। कर्णेन्द्रियों की सूक्ष्म चेतना में ही उसे अनुभव किया जा सकता है।
चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस स्तर की बनाना चाहिए कि उसे श्वाँस लेते समय 'सो' शब्द के ध्वनि प्रवाह की मन्द अनुभूति होने लगे। उसी प्रकार जब साँस छोड़ना पड़े तो यह मान्यता परिपक्व करनी चाहिए कि ‘हम् 'ध्वनि प्रवाह विनिर्मित हो रहा है। आरम्भ में कुछ समय यह अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं होती किन्तु क्रम और प्रयास जारी रखने पर कुछ ही समय उपरान्त इस प्रकार का ध्वनि प्रवाह अनुभव में आने लगता है और उसे सुनने में न केवल चित्त ही एकाग्र होता है, वरन् आनन्द का अनुभव होता है।
'सो' का तात्पर्य परमात्मा और हम् का जीव चेतना समझा जाना चाहिए। निखिल विश्व ब्रह्माण्ड में संव्याप्त महाप्राण नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अंग-प्रत्यंग में जीवकोश तथा नाड़ी तन्त्र में प्रवेश करके उसको अपने सम्पर्क संसर्ग का लाभ प्रदान करता है। यह अनुभूति ‘सो' शब्द ध्वनि के साथ अनुभूति भूमिका में उतरनी चाहिए और ‘हम' शब्द के साथ जीव भाव द्वारा इस काय-कलेवर पर से अपना कब्जा छोड़कर चले जाने की मान्यता प्रगाढ़ की जानी चाहिए।
प्रकारान्तर से परमात्म सत्ता का अपने शरीर और मनःक्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाने की ही यह धारणा है। जीव भाव अर्थात् स्वार्थवादी संकीर्णता काम, क्रोध, लोभ, मोह, भरी मद मत्सरता अपने को शरीर या मन के रूप में अनुभव करते रहने वाली आत्मा की दिग्भ्रान्त स्थिति का नाम ही जीव भूमिका है। इस भ्रम- जंजाल भरे जीव- भाव को हटा दिया जाये तो फिर अपना विशुद्ध अस्तित्व ईश्वर के अविनाशी अंश आत्मा के रूप में ही शेष रह जाता है। काय कलेवर के कण-कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना और जीव धारण की बेदखली यही है सोऽहम् साधना का तत्वज्ञान। श्वाँस-प्रश्वाँस क्रिया के माध्यम से सो और हम ध्वनि के सहारे इसी भाव-चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है। अब शरीर और मन पर से लोभ-मोह का, वासना-तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है और उसके स्थान पर उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व के रूप में ब्रह्यसता की स्थापना हो रही है। शासन परिवर्तन जैसी यह भाव भूमिका है, जिसमें अनाधिकारी-अनाचारी शासनसत्ता का तख्ता उलटकर उस स्थान पर सत्य, न्याय और प्रेम के संविधान वाली धर्मसत्ता का राज्याभिषेक किया जाता है। सोऽहम् साधना इसी अनुभूति स्तर को क्रमश प्रगाढ़ करती चली जाती है, और अन्तःकरण यह अनुभव करने लगता है कि अब उस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा, उसका समग्र संचालन देव सत्ता द्वारा किया जा सकता है।
श्वाँस ध्वनि ग्रहण करते समय ‘सो' और निकालते समय 'हम' की धारणा में लगना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि इन शब्दों के आरम्भ में अति मन्द स्तर की होने वाली अनुभूति में क्रमश: प्रखरता आती चली जाये। चिंतन का स्वरूप यह होना चाहिए कि साँस में घुले हुए भगवान अपनी समस्त विभूतियों और विशेषताओं के साथ काय-कलेवर में भीतर प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश मात्र आवागमन नहीं है वरन् प्रत्येक अवयव पर सघन आधिपत्य बन रहा है। एक-एक करके शरीर के भीतरी प्रमुख अंगों के चित्र की कल्पना करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि उसमें भगवान की सत्ता चिरस्थाई रूप से समाविष्ट हो गई। हृदय फुफ्फुस आमाशय, आँतें, गुर्दे, जिगर, तिल्ली आदि में भगवान का प्रवेश हो गया। रक्त के साथ प्रत्येक नस-नाड़ी और कोशिकाओं पर भगवान ने अपना शासन स्थापित कर लिया। बाह्य अंगों ने, पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच ज्ञानेन्द्रियों, ने भगवान के अनुशासन में रहना और उनका निर्देश पालन करना स्वीकार कर लिया। जीभ वही बोलेगी जो ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक हो। देखना, सुनना, बोलना, चलना आदि इन्द्रियजन्य गतिविधियाँ दिव्य निर्देशों का ही अनुगमन करेंगी। ज्ञानेन्द्रिय का उपयोग वासना के लिए नहीं मात्र ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए अनिवार्य आवश्यकता का धर्म संकट सामने आ खड़ा होने पर ही किया जायेगा। हाथ-पाँव मानवोचित कर्तव्य पालन के अतिरिक्त ऐसा कुछ न करेंगे जो ईश्वरीय सत्ता को कलंकित करता हो। मस्तिष्क ऐसा कुछ न सोचेगा जिसे उच्च आदर्शों के प्रतिकूल ठहराया जा सके। बुद्धि कोई अनुचित न्याय विरुद्ध एवं अदूरदर्शी-अविवेक भरा निर्णय न करेगी। चित्त में अवांछनीय एवं निकृष्ट स्तरीय आकांक्षायें न जमने पायेंगी। अहंता का स्तर नर कीटक जैसा नर-नारायण जैसा होगा।
यही हैं वे भावनायें जो शरीर और मन पर भगवान का शासन स्थापित होने के तथ्य को यथार्थ सिद्ध कर सकती हैं। यह सब उथली कल्पनाओं की तरह मनोविनोद भर नहीं रह जाना चाहिए वरन् उसकी आस्था इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि इस भाव परिवर्तन को क्रिया रूप में परिणत हुए बिना चैन ही न पड़े। सार्थकता उन्हीं विचारों की है जो क्रिया रूप में परिणत होने की प्रखरता से भरे हों।सोऽहम् साधना के पूर्वार्द्ध में अपने काय-कलेवर पर श्वसन क्रिया के साथ प्रविष्ट हुए महाप्राण की, परब्रह्म की सत्ता स्थापना का इतना गहन चिंतन करना पड़ता है कि यह कल्पना स्तर की बात न रहकर एक व्यवहारिक यथार्थता के, प्रत्यक्ष तथ्य के रूप में प्रस्तुत- दृष्टिगोचर होने लगे।
इस साधना का उत्तरार्द्ध पाप निष्कासन का है। शरीर में से अवांछनीय इन्द्रिय लिप्साओं का, आलस्य- प्रमाद जैसी दृष्प्रवृतियों का, मन से लोभ-मोह जैसी तृष्णाओं का, अन्तःस्थल से जीवभावी अहन्ता का निवारण-निराकरण हो रहा है। ऐसी भावनाएँ अत्यन्त प्रगाढ़ होनी चाहिए। दुर्भावनाएँ और दुष्कृतियाँ, निकृष्टताएँ और दुष्टताएँ और हीनताएँ सभी निरस्त हो रही हैं, सभी पालयन कर रही हैं- यह तथ्य हर पड़ी सामने दीखना चाहिए। अनुपयुक्तताओं के निरस्त होने के उपरान्त जो हलकापन, जो सन्तोष, जो उल्लास स्वभावत: होता है और निरन्तर बना रहता है, उसी का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। तभी यह कहा जा सकेगा कि सोऽहम् साधना का उत्तरार्द्ध भी एक तथ्य बन गया।
सोऽहम् साधना के पूर्व भाग में श्वाँस लेते समय ‘सो' ध्वनि के साथ जीवन सत्ता पर उस परब्रह्म परमात्मा का शासन- आधिपत्य स्थापित होने की स्वीकृति है। उत्तरार्द्ध में 'हम' को, अहंता को विसर्जित करने का भाव है। साँस निकलने के साथ-साथ अहम् भाव का भी निष्कासन हुआ। अहंता ही लोभ और मोह की जननी है। शरीराभ्यास में जीव उसी की प्रबलता के कारण डूबता है। माया, अज्ञान, अन्धकार, बन्धन आदि की भ्रान्तियाँ एवं विपत्तियाँ इस अहंता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसे विसर्जित कर देने पर ही भगवान का अन्त:क्षेत्र में प्रवेश करना, निवास करना सम्भव होता है।
इस छोटे से मानवी अन्तःकरण में दो के निवास की गुंजायश नहीं पूरी तरह एक ही रह सकता है, दोनों रहे तो लड़ते-झगड़ते रहते हैं और अन्तर्द्वन्द की खींचतान चलती रहती है। भगवान को बहिष्कृत करके पूरी तरह 'अहमन्यता' को प्रबल बना लिया जाय तो मनुष्य दुष्ट- दुर्बुद्धि, क्रूरकर्मा, असुर बनता है। अपनी कामनाएँ, भौतिक महत्त्वाकाँक्षाएँ, ऐषणाएँ समाप्त करके ईश्वरीय निर्देशों पर चलने का संकल्प ही आत्म-समर्पण है। यही शरणागति है, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त होते ही मनुष्य में देवत्व का उदय होता है, तब ईश्वरीय अनुभूतियाँ चिंतन में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता भर देती है। ऐसे ही व्यक्ति महामानव, ऋषि, देवता एवं अवतार के नाम से पुकारे जाते हैं। ‘सो' में भगवान का शासन आत्मसत्ता पर स्थापित करने और हम' में अहंता का विसर्जन करने का भाव है। प्रकारान्तर से इसे महान् परिवर्तन का, आंतरिक कायाकल्प का बीजारोपण कह सकते हैं। सोऽहम् साधना का यही है भावनात्मक एवं व्यावहारिक स्वरूप।
सोऽहम् साधना में 'अ' की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। आरम्भ में उस हृदय-चक्र स्थिति बिन्दु को ‘सो' ध्वनि के समय ब्रह्म माना जाता है और पीछे उसी की 'हं' धारणा में जीव भावना हो जाती हैं। बस भाव परिवर्तन के लिए 'अ' का अवकाश काल रखा गया है इसी प्रकार जब 'हं' समाप्त हो जाय, वायु बाहर निकल जाय और नया वायु प्रवेश करे उस समय भी दीन-भाव हटाकर उस तेज बिन्दु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। वह दोनों ही अवकाश 'अऽऽ ऽ' के समान हैं, इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। शब्द तो सो'ऽहं' का ही होता है।
‘सो' ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है। 'ऽ' प्रकृति का प्रतिनिधि है। 'हं' जीव का प्रतीक हैं। ब्रह्म, प्रकृति और जीव का सम्मिलन इस अजपा-जाप में होता है। सोऽहम्- साधना में तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म-जागरण का स्वर्ण सुयोग एक साथ ही उपलब्ध होने लगता है।
सोहम्' साधना की उन्नति जैसे-जैसे होती जाती है वैसे ही वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता जाता है। आत्म-ज्ञान बढ़ता है और धीरे-धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चलती है। आगे चलकर साँस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय स्थित सूर्य-चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हैं। उस समय समाधि की सी अवस्था हो जाती है। हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है।
स्वामी विवेकानन्द ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिए ''आत्मानुभूति'' की विधि बताई है। उनके अमेरिकन शिष्य रामाचरक ने इस विधि को ‘मेण्टल डेवलपमेण्ट ' नामक पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखा है।
Versions
-
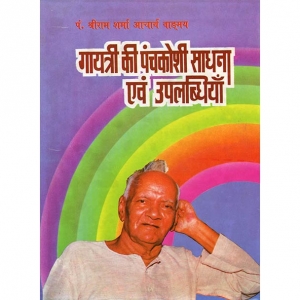
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-1Scan Book Version
-
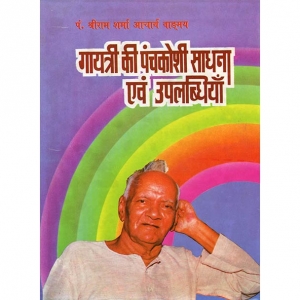
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियाँ भाग-2Scan Book Version
-
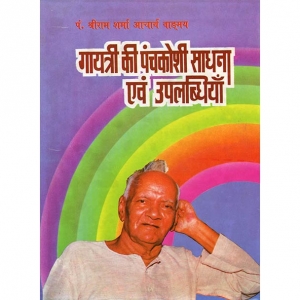
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-3Scan Book Version
-
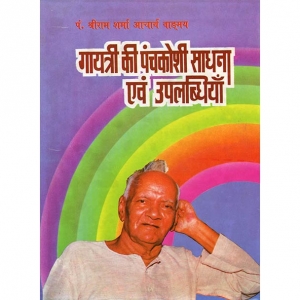
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-4Scan Book Version
-
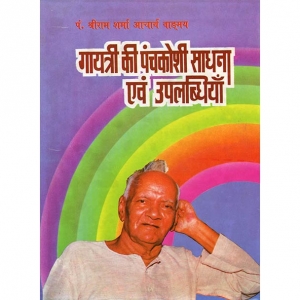
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-5Scan Book Version
-
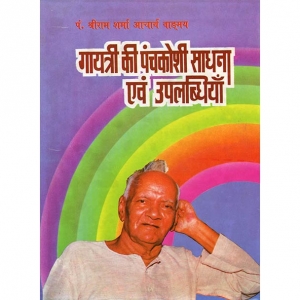
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां भाग-6Scan Book Version
-
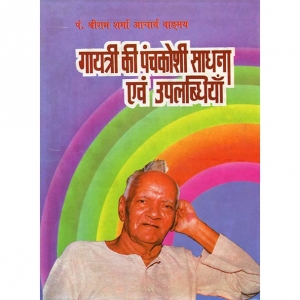
HINDIगायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियांText Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री साधना के दो स्तर
- उच्चस्तरीय साधना और उसकी सिद्धि
- उच्चस्तरीय साधना का तत्त्वज्ञान
- गायत्री के पाँच मुख
- देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य
- गायत्री माता की दस भुजायें और उनका रहस्य
- प्रतीक का निष्कर्ष
- गायत्री का भावनात्मक एवं वैज्ञानिक महत्व
- गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोश
- अनन्त आनन्द की साधना
- पाँच कोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया
- पाँच कोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि
- चेतना के पाँच आयाम पंच कोश उपासना
- सूक्ष्म शरीर के पाँच कोश एवं उनका वैज्ञानिक विवेचन
- मानवी काया की चेतनसत्ता का वैज्ञानिक विवेचन वैज्ञानिक अध्यात्मवाद
- पंच कोश और उनका अनावरण
- जीवात्मा के तीन शरीर और उनकी साधना
- तीन शरीर और उनका कार्य क्षेत्र
- कायसत्ता के तीन कलेवर एवं उनका अनावरण
- चारों ओर बिखरा सूक्ष्म का सिराजा
- अन्तराल में समाई दिव्य शक्तियाँ सिद्धियाँ
- मनुष्य देह में भरा विलक्षण विराट
- स्थूल शरीर का परिष्कार कर्मयोग से
- सूक्ष्म शरीर की महती सामर्थ्य
- सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा और उसकी विशिष्ट क्षमता
- प्रमाणित तो होता है, सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व
- सूक्ष्म शरीर के अविज्ञात क्रिया कलाप
- सूक्ष्मीकरण की अनेक गुनी सामर्थ्य
- सूक्ष्म शरीर का दिव्यीकरण
- सूक्ष्म शरीर के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि
- सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष ज्ञानयोग से
- भाव संवेदनाओं का भाण्डागार: कारण शरीर
- कारण शरीर देव शरीर
- कारण शरीर की विशिष्टता भाव श्रद्धा
- कारण शरीर का उत्कर्ष भक्तियोग से
- स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म और कारण
- योग साधना की तीन धाराएँ
- त्रिविध शरीरों की समन्वित साधना
- हमारा अद्भुत विलक्षण अन्नमय कोश
- जीव सत्ता की प्रचण्ड शक्ति सामर्थ्य
- अन्नमय कोश और चमत्कारी हार्मोन ग्रन्थियाँ
- हमारे शरीर के रहस्यमय घटक जीन्स
- अन्नमय कोश का परिष्कार और प्रतिफल
- अन्नमय कोश और उसका अनावरण
- अन्नमय कोश की जाग्रति, आहार शुद्धि से
- आहार के त्रिविध स्तर, त्रिविध प्रयोजन
- आहार, संयम और अन्नमय कोश का जागरण
- आहार विहार से जुड़ा है मन
- आहार और उसकी शुद्धि
- आहार शुद्धौः सत्व शुद्धौः
- अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति
- उपवास का आध्यात्मिक महत्त्व
- उपवास से सूक्ष्म शक्ति की अभिवृद्धि
- उपवास से उपत्यिकाओं का शोधन
- उपवास के प्रकार
- उच्चस्तरीय गायत्री साधना और आसन
- आसनों का काय विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रभाव
- आसनों के प्रकार
- सूर्य नमस्कार की विधि
- पंच तत्वों की साधना तत्व साधना एक महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म विज्ञान
- तत्व शुद्धि
- तपश्चर्या से आत्मबल की उपलब्धि
- आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है
- तपस्या का प्रचण्ड प्रताप
- तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का उद्भव
- ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- प्राणमय कोश और उसका विकास
- प्राण शक्ति का स्वरूप और अभिवर्धन
- प्राणमय कोश में सन्निहित प्रचण्ड जीवनी शक्ति-प्राण
- प्राणायाम और प्राणशक्ति
- प्राणायाम से प्राणमय कोश का परिष्कार
- प्राणमय-कोश की साधना
- प्राणाकर्षण की क्रियायें
- पाँच प्राणों की साधना-पाँच कोशों की सिद्धि
- पाँच प्राण-पाँच उपप्राणों की अद्भुत शक्ति धाराएँ
- मूल बंध, उड्डियान बंध और जालंधर बंध का रहस्य
- मुद्रा उपचार
- नौ प्राणायाम
- मनोमय कोश का अनावरण
- मनोमय कोश का विकास परिष्कार
- मनोमय कोश की साधना से सर्वार्थ सिद्धि
- मन और उसका निग्रह
- ध्यान
- त्राटक
- त्राटक-साधन से एकाग्रता शक्ति का अभिवर्द्धन
- मनोमय कोश और आज्ञा चक्र
- त्राटक साधना से दिव्य दृष्टि की जागृति
- जप साधना
- पंच तन्मात्राओं की साधनाएँ तथा सिद्धियाँ
- पंच तन्मात्राओं का पंच ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्ध
- शब्द साधना
- रूप साधना
- छाया पुरुष- हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर
- रस साधना
- गन्ध साधना
- स्पर्श- साधना
- विज्ञानमय कोश का जागरण
- विज्ञानमय कोश-सूक्ष्म सिद्धियों का केन्द्र
- विज्ञानमय कोश का केन्द्र संस्थान हृदयचक्र
- विज्ञानमय कोश और जीवन साधना
- विज्ञानमय कोश का जागरण
- सोऽहम् साधना
- आत्मानुभूति-योग
- आत्मदर्शन की समर्थ साधना
- आत्म- चिन्तन की साधना
- दूसरी साधना
- स्वर योग
- आत्मानुभूति-योग
- स्वर बदलना
- स्वर-संयम से दीर्घ जीवन
- विज्ञानमय-कोश की वायु साधना
- त्रिविधि बंधन और उनसे मुक्ति
- ग्रन्थि- बेध
- आनन्दमय कोश का अनावरण
- आनन्दमय कोश-शिव शक्ति का संगम
- २७ समाधियों में सर्वोत्तम सहज समाधि
- आनन्दमय कोश अनावरण
- नाद साधना
- नाद साधना का क्रमिक अभ्यास
- आनन्दमय कोश की तीन उपलब्धियाँ समाधि, स्वर्ग और मुक्ति
- बिन्दु साधना
- नादयोग- दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान
- बिन्दुभेद की साधना-विधि
- कला- साधना
- पाँचकलाओं द्वारा तात्विक साधना
- तुरीय अवस्था

