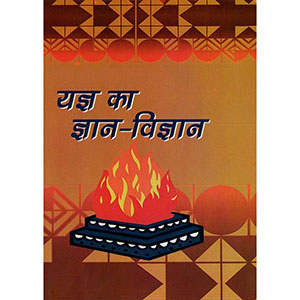यज्ञ का ज्ञान विज्ञान 
यज्ञ द्वारा तीनों ऋणों से मुक्ति
स्थूल यज्ञ में देव- पूजा इसलिए भी की जाती है कि देव तत्वों, देव आदर्शों, देव गुणों एवं देव कर्मों की ओर अभिरुचि एवं प्रवृत्ति बढ़े ।। पूजा के पीछे कोई भावना न हो, कोई उद्देश्य एवं आदर्श न हो, तब तो वह देव- पूजा का एक अन्धपरम्परा मात्र रह जायेगी ।। ऐसी पूजा से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता ।।
कोई व्यक्ति किसी सत्पुरुष के दर्शन को तो दौड़ा जाय पर उसकी शिक्षाओं पर ध्यान न दें तो उस दर्शन- मात्र से उसे क्या लाभ होगा? जिस महापुरुष के प्रति उसे श्रद्धा है, उसकी शिक्षाओं का तथा विशेषताओं का अनुकरण किया जाय, तो बिना दर्शन के भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।। अनेकों रूढ़िवादी- अंधविश्वासी केवल देव- पूजा का कर्म काण्ड करके अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं ।। देवत्व को अपने में धारण करना देव- पूजन का प्रधान उद्देश्य है ।।
यदि हमारे विचार और कार्य असुरता से भरे हुए हैं, तो देव- पूजन करने की चिह्न पूजा से क्या लाभ? अध्यात्म- यज्ञ में अपनी अन्तरात्मा में देवतत्वों का आवाहन किया जाता है और दैवी सम्पदाओं से अपने को परिपूर्ण बनाया जाता है ।।
गीता के 16 वें अध्याय में सद्भावनाओं, सद्गुणों और सत्व कार्यों के 26 लक्षणों को दैवी सम्पदा में बताया गया है ।। जिनमें इन तत्वों की अधिकता होने लगे, समझना चाहिए कि वह देव उपासक है ।। इसके विपरीत लक्षणों वाला व्यक्ति चाहे वह कितने ही विधि- विधान सहित देव- पूजा करता हो- देव- पूजक होते हुए भी असुर रहने वाले रावण की तरह निन्दनीय ठहराया जायगा ।। अध्यात्म यज्ञ की देव- पूजा का वास्तविक तात्पर्य अपने में देवत्व की अभिवृद्धि करना ही है ।।
अग्नि- पूजा का आध्यात्मिक मर्म कर्तव्य निष्ठा है ।। अपने धर्म- मार्ग को न छोड़ना, कर्तव्य धर्म रूपी हवन में अपना सब कुछ झोंक देना, होम देना ही सच्चा अग्नि पूजन है ।।
अपने आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में मनुष्य को सदैव जागरूक रहना चाहिए ।। अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, समस्त प्राणधारियों के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन्हें पूरा करने में दत्त चित्त रहना, यज्ञ भावना का ही प्रतीक है ।।
यजुर्वेद २ ।। १३१ में पितृ- यज्ञ का वर्णन है ।। इसका तात्पर्य है, पितृजनों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना ।। पिता को गार्हपत्याग्नि, माता को दक्षिणाग्नि- आचार्य को आह्वनीय अग्नि कहा गया है ।। इन तीन अग्नियों में पितृ- यज्ञ किया जाता है ।। इसका तात्पर्य है, इन तीनों का आदर करना, इनकी सामर्थ्यों को बढ़ाने के लिए सहयोग देना, तथा इनका आज्ञानुवर्ती होना ।। यही सच्चा पितृ- यज्ञ है ।।
इसी प्रकार मनुष्य जाति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नरमेध, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्यों का पालन करना अश्वमेध, अपनी इन्द्रियों को कुमार्ग- गमन से बचाकर सन्मार्ग में लगा देना गो मेध, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक तथा सांसारिक समस्त सम्पदाओं को लगा देना सर्वमेध है, इन्हीं महान यज्ञों तक यजमान को पहुँचाना अग्निहोत्र का प्रधान लक्ष्य है ।।
यज्ञ में भावना ही प्रधान है ।।
जैसी उच्च या निकृष्ट भावना से कोई कर्म किया जाता, उसके अनुकूल ही उसका परिणाम मिलता है ।। कोई कार्य बाह्य दृष्टि से कितना ही उत्तम क्यों न दिखता हो, पर यदि उसके पीछे नीच उद्देश्य छिपा हुआ है, तो उसका कोई अच्छा परिणाम न होगा ।। भावना की निकृष्टता के कारण विष मिले हुए दूध के समान वह गन्दा हो जायेगा ।।
इसके विपरीत यदि उच्च भावना से प्रेरित होकर कोई ऐसा कार्य भी करना पड़े, जो देखने में निन्दनीय प्रतीत होता हो, तो भावना की उत्कृष्टता के कारण वह भी शुभ फलदायक होता है ।।
डॉक्टर का फोड़ा चीरना- एक निष्ठुर कार्य प्रतीत होता है, पर उसके मन में रोगी का दुःख दूर करने की भावना है ।। इसलिए वह चीर- फाड़ की निष्ठुरता भी दया ही है ।। इसी प्रकार बहेलिये का चिड़ियों को दाना फेंकना चाहे, बाहरी आँखों से दान या दया का कृत्य भले ही दिखे, पर उसका वास्तविक उद्देश्य चिड़ियों को पकड़ना है, इसलिए वह दाना- फेंकना भी उसकी अधोगति का ही कारण बनता है ।।
गीता में भावना की प्रधानता को ध्यान में रखकर अन्य कर्मों की भाँति यज्ञ को भी सात्विक, राजस, तामस अर्थात् उत्तम, मध्यम, निकृष्ट विभागों में बाँटा है-
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते ।।
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः॥ गीता १७/११
जो यज्ञ, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा उसे करना कर्तव्य ही है, ऐसा मानकर, फल, को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है ।।
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥ गीता १७१२
जो यज्ञ केवल प्रदर्शन के लिए, अथवा फल को भी लख रख कर किया जाता है, उसे हे अर्जुन ! तू राजस जान ।।
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ गीता १७/१३
शास्त्र- विधि से हीन, अन्न- दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किये हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं ।।
इन यज्ञों का फल उनके बाह्य रूप के अनुसार नहीं, वरन् कर्त्ता की भावना के अनुसार होता है ।।
र्उध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ गीता १७/१४
सतगुण में स्थित हुए मनुष्य ऊपर उठते हैं, उच्च गति को प्राप्त करते हैं, रजोगुण में स्थित बीच में ही लटकते रहते हैं, तथा निकृष्ट मार्ग पर चलने वाले तामस मनुष्य अधोगामी होते हैं ।।
क्रिया- यज्ञ में विधि- विधान के शास्त्रोक्त होने की ध्यान रखा जाता है और भाव- यज्ञ में आन्तरिक भावना की पवित्रता, सात्विकता, सच्चाई एवं सदुद्देश्य को महत्त्व दिया जाता है ।। उच्च भावना रखकर किये जाने वाले साधारण कार्य भी यज्ञ- रूप हो जाते हैं ।।
मनुष्य सामाजिक प्राणी है ।। वह स्वयं ही अपनी सब जरूरतें पूरी नहीं कर लेता, वरन् अनेक व्यक्तियों, पशुओं, वृक्षों, वनस्पतियों तथा ईश्वरीय शक्तियों की सहायता से उसका जीवन- क्रम चलना संभव होता है ।। यदि दूसरों को सहयोग उसे न मिले, तो उसका काम एक क्षण के लिए भी न चले, यहाँ तक कि जीवन- धारण करना भी दुर्लभ हो जाय ।। अन्न, वस्त्र, औषधि, घर, जूते, पुस्तक आदि वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए सहस्रों दूसरों का सहयोग नित्य अपेक्षित होता है ।।
जो ज्ञान, विद्या, शिक्षा, स्वभाव, पद, कीर्ति आदि हमें उपलब्ध हैं वह भी दूसरों के सहयोग से ही हैं ।। गर्भ में आने के समय से लेकर चिता में जलने तक हर घड़ी मनुष्य दूसरों के सहयोग, कृपा- भाव, दान, अनुग्रह प्राप्त करता रहता है ।। इसलिए उसे उचित है, कि इन ऋणों से अपने को उऋण करने के लिये कृतज्ञता- पूर्वक संसार की सेवा करे ।। अपने ऊपर लदे हुए दूसरों से असंख्य उपकारों का ऋण चुका कर उऋण होने का प्रयत्न करे ।। शास्त्र का भी ऐसा ही आदेश हैः -
जायमानो वै ब्राह्मणास्त्रिभिर्ऋर्णऋर्णवान् जायते ।।
ब्रह्मचयेर्ण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजयापितृभ्यः॥ तैत्तिरीय संहिता ३/१०/५
द्विज, जन्मते ही ऋषि- ऋण, देवऋण, और पितृऋण इन तीन प्रकार के ऋणों से ऋणी बन जाता है ।। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषिऋण से, यज्ञ द्वारा देवऋण से और सन्तति को सुयोग्य बनाने से पितृऋण से छुटकारा मिलता है ।।
ऋषि, देव, पितृ हमारे ऊपर अनन्त कृपा- पूर्वक हमें बहुत कुछ देते हैं ।। सद्ज्ञान ऋषियों का दिया हुआ है ।। अनेक साधन सामग्री तथा सुखोपभोग की सामग्री देवों द्वारा दी हुई है ।। असमर्थ अवस्था में सामर्थ्य प्रदान करने वाले वे उपकार पृत्रो के हैं, जिनके द्वारा सब प्रकार से दीन- हीन नवजात शिशु पाला- पोसा जाता है और अन्त में सब प्रकार की सामर्थ्यों से परिपूर्ण मनुष्य बन जाता है ।। इन दोनों के उपकार प्राप्त न हों, तो मनुष्य की कैसी दुर्गती हो इसकी कल्पना करना भी कठिन है ।।
इन ऋणों से उऋण हुए बिना कोई व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता ।।
जो लोग दूसरों का कर्ज मारने की चेष्टा करते हुए 'विरक्त' बनने का ढोंग रचते हैं, वे वस्तुतः कृतघ्न हैं ।। उन्हें मुक्ति तो क्या मिलेगी, उल्टे हजारों गुने जटिल बंधन पाश में बँधना पड़ेगा ।। साधु या संन्यासी तो ईश्वर उपासना करते हुए अधिकाधिक लोग- सेवा करने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ते हैं ।।
स्वार्थपरता को न छोड़कर कर्तव्य- पालन एवं लोक- सेवा द्वारा उऋण होने की कठिनाई या मेहनत से जी चुराकर जो आलस्य और हराम- खोरी पर उतर आते हैं और कहते हैं संसार तो माया है, दूसरों के लिए हम कोई प्रयत्न क्यों करें, ऐसे लोगों को साधु महात्मा या त्यागी बैरागी कहना भी इन पवित्र शब्दों को कलंकित करना है ।।
साधु वह है- जो अपना ऋण दूसरों पर छोड़े, जो स्वयं सबका कर्जदार बैठा है और बदला चुकाने के समय कतराता है, वह तो पक्का चोर है ।। उसे न तो साधु कह सकते हैं और न साधु ।। प्रत्येक व्यक्ति को उपरोक्त तीन ऋणों से उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए ।। इस उऋणता के उपाय तैत्तरीय संहिता के उपरोक्त वाक्य में बता दिये गये हैं ।।
(१) ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषि- ऋण से छुटकारा मिलता है ।। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री- सम्भोग न करना ही नहीं है, वरन् उसका वास्तविक तात्पर्य सभी इन्द्रियों का संयम करना और ब्रह्म में चरण रखना अर्थात आस्तिकता को अपनाना है ।।
इन्द्रियों के संयम से, शारीरिक और मानसिक शक्तियों की रक्षा होती है और असंयमी आचरण के कारण जो समय, धन, स्वास्थ्य एवं आत्मबल नष्ट होता है, वह बच जाता है ।। इस असंयम से बचे हुए और संयम द्वारा बड़े हुए बल को जब मनुष्य आस्तिकता में धर्म- मार्ग में लगता है, उसकी सर्वांगीण उन्नति होती है ।।
ऋषि स्वयं महान होते हैं, हमें भी ऋषि- ऋण से मुक्त होने के लिए अपने को ज्ञान, धर्म, संगठन आदि सभी दृष्टियों से बलवान बनाना चाहिये ।। ऋषि, पक्ष की परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिये अपने को आदर्श एवं उदाहरण के रूप में उपस्थित कर सकें ।।
(२) देव ऋण से छुटकारा यज्ञ द्वारा होता है ।। यज्ञ देव- शक्तियाँ परिपुष्ट कैसे होती हैं, उसका विज्ञान पीछे बताया जा चुका है ।। अध्यात्म क्षेत्र में यज्ञ का अर्थ है त्याग ।। अपने निवारण के लिए अपनी सामर्थ्य का न्यूनतम भाग उपभोग करना और अधिकतम भाग लोकहित के लिए लगा देना यही यज्ञ भावना है ।।
देव हमें नाना प्रकार के सुख- साधन देते हैं हमें किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए? अवश्य ही देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए 'देव' वे कहलाते हैं कि जो देते हैं ।। देने वालों की श्रेणी में अपने को रखने से भी हम देव बन सकते हैं ।।
धन- देना ही दान नहीं है ।। ज्ञान, समय, श्रम, सलाह, सद्भाव, शिक्षा, सहयोग आदि देकर हम अपनी स्थिति के अनुसार दूसरों को बहुत कुछ देते रह सकते हैं ।। देने की भावना हो, तो प्रतिक्षण वैसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं ।। ऋषि- मुनि तो पूर्णतया निर्धन होते थे, पर वे इतना देते थे कि उनके दान की तुलना धन कुबेर भी नहीं कर सकते ।।
देने की किन्तु विवेक पूर्वक देना की भावना से हम देव ऋण से मुक्त होते हैं किन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कायर एवम् पात्र- कुपात्र का विचार न किया जाय, तो वह दान हत्या के समान भयन्कर दुःखदायी भी होता है ।। इसलिए देव श्रद्धा से छुटकारा पाने के लिए विवेक पूर्ण त्याग करते रहने का हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए ।।
(३) तीसरा ऋण है- पितृ- ऋण ।। पितर हमें सुयोग बनाते हैं ।। हम भी भावी सन्तान को सुयोग बनावें ।। आज के युग में अधिक बच्चे पैदा करना एक राष्ट्रीय पाप है ।। क्योंकि जब जनसंख्या की अधिकता से अन्न का पूरा न पड़ता हो, अन्न के अभाव से अनेक लोग भूखों मरते हों, तब उनके ग्रास छीनने के लिए और नये हिस्सेदार बढ़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं है ।। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, वरन् उनकी योग्यता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ।। भावी पीढ़ी के उचित निर्माण के लिए ध्यान न दिया जायेगा, तो भविष्य अन्धकारमय बनेगा ।।
आज कुसंस्कारों की बढ़ोत्तरी से नयी पीढ़ियाँ, उद्दण्डता, उच्छृंखलता, अवज्ञा, आलस, विलासिता आदि बुराइयों की ओर बढ़ रही हैं ।। इस बाढ़ को न रोका गया तो, भविष्य का ईश्वर ही मालिक है ।। इसलिए बच्चों को भविष्य के सुयोग्य नागरिक एवं महान सत्पुरुष बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए पितृ- ऋण से उऋण होना चाहिए ।। अपने या पराये, जिन बच्चों की ऐसी सेवा की जाय, वह पितृ- ऋण की उऋणता ही है ।।
पितर का अर्थ गुरु भी है ।। जिस प्रकार सत्पुरुषों ने हमें सद्ज्ञान दिया और अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए अनेक प्रकार प्रयत्न किये, वैसे ही हमारे लिए उचित है, कि दूसरों को सद्ज्ञान देने और सत्- मार्ग पर लगाने के लिए प्रयत्न करें ।। यह पितृ- परम्परा जारी रखने की भावना सब की हो, तो दूसरों को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हुए सम्पूर्ण विश्व को सुयोग बनाया जा सकता है ।।
तीनों ऋणों से उऋण होने के लिये हममें से प्रत्येक को ध्यान रखना चाहिए ।। ऋषि, देव और पितृ भी इस यज्ञ- भावना से प्रेरित होकर कायर करते हैं ।। उनका यज्ञ यह यज्ञ- भावना ही है ।। इसी को यज्ञ से यज्ञ करना कहते हैं ।। देवों की महानता इस यज्ञों के यज्ञ- आध्यात्मिक यज्ञ पर निर्भर थी ।। इसी से वे इतने उच्च अधिकारी बने ।।
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमार्णि प्रथमान्यासन् ।।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पवेर् साध्याः सन्ति देवाः॥ -यजुर्वेद
देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया, जो प्रथम धर्म था ।। इसी से वे उस महान् स्वर्ग को गये, जहाँ पूर्व काल में ऋषि गये हैं ।।
देवों ने हमें मार्ग दिखाया ।। हमारा कर्तव्य है कि इस यज्ञ मार्ग पर चलते हुए उस महान परम्परा को कायम रखें और उऋणता का आत्म- सन्तोष प्राप्त करते हुए जीवन के महान लक्ष्य को उपलब्ध करें ।।
(यज्ञ का ज्ञान- विज्ञान पृ. 3.21- 22)
कोई व्यक्ति किसी सत्पुरुष के दर्शन को तो दौड़ा जाय पर उसकी शिक्षाओं पर ध्यान न दें तो उस दर्शन- मात्र से उसे क्या लाभ होगा? जिस महापुरुष के प्रति उसे श्रद्धा है, उसकी शिक्षाओं का तथा विशेषताओं का अनुकरण किया जाय, तो बिना दर्शन के भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।। अनेकों रूढ़िवादी- अंधविश्वासी केवल देव- पूजा का कर्म काण्ड करके अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं ।। देवत्व को अपने में धारण करना देव- पूजन का प्रधान उद्देश्य है ।।
यदि हमारे विचार और कार्य असुरता से भरे हुए हैं, तो देव- पूजन करने की चिह्न पूजा से क्या लाभ? अध्यात्म- यज्ञ में अपनी अन्तरात्मा में देवतत्वों का आवाहन किया जाता है और दैवी सम्पदाओं से अपने को परिपूर्ण बनाया जाता है ।।
गीता के 16 वें अध्याय में सद्भावनाओं, सद्गुणों और सत्व कार्यों के 26 लक्षणों को दैवी सम्पदा में बताया गया है ।। जिनमें इन तत्वों की अधिकता होने लगे, समझना चाहिए कि वह देव उपासक है ।। इसके विपरीत लक्षणों वाला व्यक्ति चाहे वह कितने ही विधि- विधान सहित देव- पूजा करता हो- देव- पूजक होते हुए भी असुर रहने वाले रावण की तरह निन्दनीय ठहराया जायगा ।। अध्यात्म यज्ञ की देव- पूजा का वास्तविक तात्पर्य अपने में देवत्व की अभिवृद्धि करना ही है ।।
अग्नि- पूजा का आध्यात्मिक मर्म कर्तव्य निष्ठा है ।। अपने धर्म- मार्ग को न छोड़ना, कर्तव्य धर्म रूपी हवन में अपना सब कुछ झोंक देना, होम देना ही सच्चा अग्नि पूजन है ।।
अपने आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में मनुष्य को सदैव जागरूक रहना चाहिए ।। अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, समस्त प्राणधारियों के प्रति जो कर्तव्य हैं, उन्हें पूरा करने में दत्त चित्त रहना, यज्ञ भावना का ही प्रतीक है ।।
यजुर्वेद २ ।। १३१ में पितृ- यज्ञ का वर्णन है ।। इसका तात्पर्य है, पितृजनों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना ।। पिता को गार्हपत्याग्नि, माता को दक्षिणाग्नि- आचार्य को आह्वनीय अग्नि कहा गया है ।। इन तीन अग्नियों में पितृ- यज्ञ किया जाता है ।। इसका तात्पर्य है, इन तीनों का आदर करना, इनकी सामर्थ्यों को बढ़ाने के लिए सहयोग देना, तथा इनका आज्ञानुवर्ती होना ।। यही सच्चा पितृ- यज्ञ है ।।
इसी प्रकार मनुष्य जाति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नरमेध, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्यों का पालन करना अश्वमेध, अपनी इन्द्रियों को कुमार्ग- गमन से बचाकर सन्मार्ग में लगा देना गो मेध, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक तथा सांसारिक समस्त सम्पदाओं को लगा देना सर्वमेध है, इन्हीं महान यज्ञों तक यजमान को पहुँचाना अग्निहोत्र का प्रधान लक्ष्य है ।।
यज्ञ में भावना ही प्रधान है ।।
जैसी उच्च या निकृष्ट भावना से कोई कर्म किया जाता, उसके अनुकूल ही उसका परिणाम मिलता है ।। कोई कार्य बाह्य दृष्टि से कितना ही उत्तम क्यों न दिखता हो, पर यदि उसके पीछे नीच उद्देश्य छिपा हुआ है, तो उसका कोई अच्छा परिणाम न होगा ।। भावना की निकृष्टता के कारण विष मिले हुए दूध के समान वह गन्दा हो जायेगा ।।
इसके विपरीत यदि उच्च भावना से प्रेरित होकर कोई ऐसा कार्य भी करना पड़े, जो देखने में निन्दनीय प्रतीत होता हो, तो भावना की उत्कृष्टता के कारण वह भी शुभ फलदायक होता है ।।
डॉक्टर का फोड़ा चीरना- एक निष्ठुर कार्य प्रतीत होता है, पर उसके मन में रोगी का दुःख दूर करने की भावना है ।। इसलिए वह चीर- फाड़ की निष्ठुरता भी दया ही है ।। इसी प्रकार बहेलिये का चिड़ियों को दाना फेंकना चाहे, बाहरी आँखों से दान या दया का कृत्य भले ही दिखे, पर उसका वास्तविक उद्देश्य चिड़ियों को पकड़ना है, इसलिए वह दाना- फेंकना भी उसकी अधोगति का ही कारण बनता है ।।
गीता में भावना की प्रधानता को ध्यान में रखकर अन्य कर्मों की भाँति यज्ञ को भी सात्विक, राजस, तामस अर्थात् उत्तम, मध्यम, निकृष्ट विभागों में बाँटा है-
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते ।।
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः॥ गीता १७/११
जो यज्ञ, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा उसे करना कर्तव्य ही है, ऐसा मानकर, फल, को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है ।।
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥ गीता १७१२
जो यज्ञ केवल प्रदर्शन के लिए, अथवा फल को भी लख रख कर किया जाता है, उसे हे अर्जुन ! तू राजस जान ।।
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ गीता १७/१३
शास्त्र- विधि से हीन, अन्न- दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किये हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं ।।
इन यज्ञों का फल उनके बाह्य रूप के अनुसार नहीं, वरन् कर्त्ता की भावना के अनुसार होता है ।।
र्उध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ गीता १७/१४
सतगुण में स्थित हुए मनुष्य ऊपर उठते हैं, उच्च गति को प्राप्त करते हैं, रजोगुण में स्थित बीच में ही लटकते रहते हैं, तथा निकृष्ट मार्ग पर चलने वाले तामस मनुष्य अधोगामी होते हैं ।।
क्रिया- यज्ञ में विधि- विधान के शास्त्रोक्त होने की ध्यान रखा जाता है और भाव- यज्ञ में आन्तरिक भावना की पवित्रता, सात्विकता, सच्चाई एवं सदुद्देश्य को महत्त्व दिया जाता है ।। उच्च भावना रखकर किये जाने वाले साधारण कार्य भी यज्ञ- रूप हो जाते हैं ।।
मनुष्य सामाजिक प्राणी है ।। वह स्वयं ही अपनी सब जरूरतें पूरी नहीं कर लेता, वरन् अनेक व्यक्तियों, पशुओं, वृक्षों, वनस्पतियों तथा ईश्वरीय शक्तियों की सहायता से उसका जीवन- क्रम चलना संभव होता है ।। यदि दूसरों को सहयोग उसे न मिले, तो उसका काम एक क्षण के लिए भी न चले, यहाँ तक कि जीवन- धारण करना भी दुर्लभ हो जाय ।। अन्न, वस्त्र, औषधि, घर, जूते, पुस्तक आदि वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए सहस्रों दूसरों का सहयोग नित्य अपेक्षित होता है ।।
जो ज्ञान, विद्या, शिक्षा, स्वभाव, पद, कीर्ति आदि हमें उपलब्ध हैं वह भी दूसरों के सहयोग से ही हैं ।। गर्भ में आने के समय से लेकर चिता में जलने तक हर घड़ी मनुष्य दूसरों के सहयोग, कृपा- भाव, दान, अनुग्रह प्राप्त करता रहता है ।। इसलिए उसे उचित है, कि इन ऋणों से अपने को उऋण करने के लिये कृतज्ञता- पूर्वक संसार की सेवा करे ।। अपने ऊपर लदे हुए दूसरों से असंख्य उपकारों का ऋण चुका कर उऋण होने का प्रयत्न करे ।। शास्त्र का भी ऐसा ही आदेश हैः -
जायमानो वै ब्राह्मणास्त्रिभिर्ऋर्णऋर्णवान् जायते ।।
ब्रह्मचयेर्ण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजयापितृभ्यः॥ तैत्तिरीय संहिता ३/१०/५
द्विज, जन्मते ही ऋषि- ऋण, देवऋण, और पितृऋण इन तीन प्रकार के ऋणों से ऋणी बन जाता है ।। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषिऋण से, यज्ञ द्वारा देवऋण से और सन्तति को सुयोग्य बनाने से पितृऋण से छुटकारा मिलता है ।।
ऋषि, देव, पितृ हमारे ऊपर अनन्त कृपा- पूर्वक हमें बहुत कुछ देते हैं ।। सद्ज्ञान ऋषियों का दिया हुआ है ।। अनेक साधन सामग्री तथा सुखोपभोग की सामग्री देवों द्वारा दी हुई है ।। असमर्थ अवस्था में सामर्थ्य प्रदान करने वाले वे उपकार पृत्रो के हैं, जिनके द्वारा सब प्रकार से दीन- हीन नवजात शिशु पाला- पोसा जाता है और अन्त में सब प्रकार की सामर्थ्यों से परिपूर्ण मनुष्य बन जाता है ।। इन दोनों के उपकार प्राप्त न हों, तो मनुष्य की कैसी दुर्गती हो इसकी कल्पना करना भी कठिन है ।।
इन ऋणों से उऋण हुए बिना कोई व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता ।।
जो लोग दूसरों का कर्ज मारने की चेष्टा करते हुए 'विरक्त' बनने का ढोंग रचते हैं, वे वस्तुतः कृतघ्न हैं ।। उन्हें मुक्ति तो क्या मिलेगी, उल्टे हजारों गुने जटिल बंधन पाश में बँधना पड़ेगा ।। साधु या संन्यासी तो ईश्वर उपासना करते हुए अधिकाधिक लोग- सेवा करने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ते हैं ।।
स्वार्थपरता को न छोड़कर कर्तव्य- पालन एवं लोक- सेवा द्वारा उऋण होने की कठिनाई या मेहनत से जी चुराकर जो आलस्य और हराम- खोरी पर उतर आते हैं और कहते हैं संसार तो माया है, दूसरों के लिए हम कोई प्रयत्न क्यों करें, ऐसे लोगों को साधु महात्मा या त्यागी बैरागी कहना भी इन पवित्र शब्दों को कलंकित करना है ।।
साधु वह है- जो अपना ऋण दूसरों पर छोड़े, जो स्वयं सबका कर्जदार बैठा है और बदला चुकाने के समय कतराता है, वह तो पक्का चोर है ।। उसे न तो साधु कह सकते हैं और न साधु ।। प्रत्येक व्यक्ति को उपरोक्त तीन ऋणों से उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए ।। इस उऋणता के उपाय तैत्तरीय संहिता के उपरोक्त वाक्य में बता दिये गये हैं ।।
(१) ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषि- ऋण से छुटकारा मिलता है ।। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री- सम्भोग न करना ही नहीं है, वरन् उसका वास्तविक तात्पर्य सभी इन्द्रियों का संयम करना और ब्रह्म में चरण रखना अर्थात आस्तिकता को अपनाना है ।।
इन्द्रियों के संयम से, शारीरिक और मानसिक शक्तियों की रक्षा होती है और असंयमी आचरण के कारण जो समय, धन, स्वास्थ्य एवं आत्मबल नष्ट होता है, वह बच जाता है ।। इस असंयम से बचे हुए और संयम द्वारा बड़े हुए बल को जब मनुष्य आस्तिकता में धर्म- मार्ग में लगता है, उसकी सर्वांगीण उन्नति होती है ।।
ऋषि स्वयं महान होते हैं, हमें भी ऋषि- ऋण से मुक्त होने के लिए अपने को ज्ञान, धर्म, संगठन आदि सभी दृष्टियों से बलवान बनाना चाहिये ।। ऋषि, पक्ष की परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिये अपने को आदर्श एवं उदाहरण के रूप में उपस्थित कर सकें ।।
(२) देव ऋण से छुटकारा यज्ञ द्वारा होता है ।। यज्ञ देव- शक्तियाँ परिपुष्ट कैसे होती हैं, उसका विज्ञान पीछे बताया जा चुका है ।। अध्यात्म क्षेत्र में यज्ञ का अर्थ है त्याग ।। अपने निवारण के लिए अपनी सामर्थ्य का न्यूनतम भाग उपभोग करना और अधिकतम भाग लोकहित के लिए लगा देना यही यज्ञ भावना है ।।
देव हमें नाना प्रकार के सुख- साधन देते हैं हमें किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए? अवश्य ही देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए 'देव' वे कहलाते हैं कि जो देते हैं ।। देने वालों की श्रेणी में अपने को रखने से भी हम देव बन सकते हैं ।।
धन- देना ही दान नहीं है ।। ज्ञान, समय, श्रम, सलाह, सद्भाव, शिक्षा, सहयोग आदि देकर हम अपनी स्थिति के अनुसार दूसरों को बहुत कुछ देते रह सकते हैं ।। देने की भावना हो, तो प्रतिक्षण वैसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं ।। ऋषि- मुनि तो पूर्णतया निर्धन होते थे, पर वे इतना देते थे कि उनके दान की तुलना धन कुबेर भी नहीं कर सकते ।।
देने की किन्तु विवेक पूर्वक देना की भावना से हम देव ऋण से मुक्त होते हैं किन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कायर एवम् पात्र- कुपात्र का विचार न किया जाय, तो वह दान हत्या के समान भयन्कर दुःखदायी भी होता है ।। इसलिए देव श्रद्धा से छुटकारा पाने के लिए विवेक पूर्ण त्याग करते रहने का हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए ।।
(३) तीसरा ऋण है- पितृ- ऋण ।। पितर हमें सुयोग बनाते हैं ।। हम भी भावी सन्तान को सुयोग बनावें ।। आज के युग में अधिक बच्चे पैदा करना एक राष्ट्रीय पाप है ।। क्योंकि जब जनसंख्या की अधिकता से अन्न का पूरा न पड़ता हो, अन्न के अभाव से अनेक लोग भूखों मरते हों, तब उनके ग्रास छीनने के लिए और नये हिस्सेदार बढ़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं है ।। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, वरन् उनकी योग्यता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ।। भावी पीढ़ी के उचित निर्माण के लिए ध्यान न दिया जायेगा, तो भविष्य अन्धकारमय बनेगा ।।
आज कुसंस्कारों की बढ़ोत्तरी से नयी पीढ़ियाँ, उद्दण्डता, उच्छृंखलता, अवज्ञा, आलस, विलासिता आदि बुराइयों की ओर बढ़ रही हैं ।। इस बाढ़ को न रोका गया तो, भविष्य का ईश्वर ही मालिक है ।। इसलिए बच्चों को भविष्य के सुयोग्य नागरिक एवं महान सत्पुरुष बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए पितृ- ऋण से उऋण होना चाहिए ।। अपने या पराये, जिन बच्चों की ऐसी सेवा की जाय, वह पितृ- ऋण की उऋणता ही है ।।
पितर का अर्थ गुरु भी है ।। जिस प्रकार सत्पुरुषों ने हमें सद्ज्ञान दिया और अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए अनेक प्रकार प्रयत्न किये, वैसे ही हमारे लिए उचित है, कि दूसरों को सद्ज्ञान देने और सत्- मार्ग पर लगाने के लिए प्रयत्न करें ।। यह पितृ- परम्परा जारी रखने की भावना सब की हो, तो दूसरों को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हुए सम्पूर्ण विश्व को सुयोग बनाया जा सकता है ।।
तीनों ऋणों से उऋण होने के लिये हममें से प्रत्येक को ध्यान रखना चाहिए ।। ऋषि, देव और पितृ भी इस यज्ञ- भावना से प्रेरित होकर कायर करते हैं ।। उनका यज्ञ यह यज्ञ- भावना ही है ।। इसी को यज्ञ से यज्ञ करना कहते हैं ।। देवों की महानता इस यज्ञों के यज्ञ- आध्यात्मिक यज्ञ पर निर्भर थी ।। इसी से वे इतने उच्च अधिकारी बने ।।
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमार्णि प्रथमान्यासन् ।।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पवेर् साध्याः सन्ति देवाः॥ -यजुर्वेद
देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया, जो प्रथम धर्म था ।। इसी से वे उस महान् स्वर्ग को गये, जहाँ पूर्व काल में ऋषि गये हैं ।।
देवों ने हमें मार्ग दिखाया ।। हमारा कर्तव्य है कि इस यज्ञ मार्ग पर चलते हुए उस महान परम्परा को कायम रखें और उऋणता का आत्म- सन्तोष प्राप्त करते हुए जीवन के महान लक्ष्य को उपलब्ध करें ।।
(यज्ञ का ज्ञान- विज्ञान पृ. 3.21- 22)
Write Your Comments Here:
- यज्ञ का ज्ञान विज्ञान
- यज्ञों के विविध प्रकार -ब्रह्मयज्ञ
- यज्ञों के प्रकार
- विशेष प्रयोजन के विशेष यज्ञ
- यज्ञीय कर्मकाण्ड प्रारम्भिक कर्मकाण्ड
- गुरु वन्दना
- सरस्वती वन्दना
- व्यास वन्दना
- साधनादिपवित्रीकरणम्
- यज्ञ-संचालन पंचोपचार पूजन पवित्रीकरणम्
- आचमनम्
- शिखावन्दनम्
- प्राणायामः
- न्यासः
- मंगलाचरणम्
- देव प्रार्थना-पृथ्वी पूजनम्
- संकल्पः
- यज्ञोपवीतपरिवर्तनम्
- चन्दनधारणम्
- रक्षासूत्रम्
- कलशपूजनम्
- कलश प्रार्थना
- दीपपूजनम्
- देवावाहनम्
- सर्वदेवनमस्कारः
- षोडशोपचारपूजनम्
- स्वस्तिवाचनम्
- रक्षाविधानम्
- अग्निस्थापनम्
- गायत्री स्तवनम्
- अग्नि प्रदीपनम्
- समिधाधानम्
- जलप्रसेचनम्
- आहुतियाँ आज्याहुतिः
- आहुतियाँ गायत्रीमन्त्राहुतिः
- आहुतियाँ स्वष्टकृत्होमः
- देवदक्षिणा- पूर्णाहुतिः
- विसर्जन वसोर्धारा
- विसर्जन -नीराजनम् - आरती
- विसर्जन -घृतावघ्राणम्
- विसर्जन -भस्मधारणम्
- विसर्जन - क्षमा प्रार्थना
- विसर्जन - साष्टांगनमस्कारः
- विसर्जन -शुभकामना
- विसर्जन -पुष्पांजलिः
- विसर्जन -शान्ति-अभिषिंचनम्
- विसर्जन -सूर्याघ्यदानम्
- विसर्जन -प्रदक्षिणा
- यज्ञों का वैज्ञानिक आधार -यज्ञ भारतीय दर्शन का ईष्ट आराध्य
- यज्ञ से संपूर्ण जगत का पालन कैसे?
- सकाम यज्ञों का रहस्य मय विज्ञान
- यज्ञ क्यों करें?
- यज्ञ से लाभ -स्वर्ग की प्राप्ति
- यज्ञकर्त्ता ऋणि नही रहता
- यज्ञ द्वारा तीनों ऋणों से मुक्ति
- पापों का प्रायश्चित
- तीर्थों की स्थापना
- सुसंन्तति की प्राप्ति
- यज्ञोपैथी-यज्ञः एक समग्र उपचार प्रक्रिया
- यज्ञोपैथी एक समग्र चिकित्सा पद्धति
- अग्निहोत्र से शरीर ही नहीं, मन का भी उपचार
- यज्ञावशिष्ट, पुरोडाश एवं चरु की महत्ता
- यज्ञ से आत्म शान्ति
- यज्ञों के विविध प्रकार -ब्रह्मयज्ञ