गायत्री महाविज्ञान 
पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य
Read Scan Version
मोटी दृष्टि से देखने पर एक शरीर के अन्दर एक जीव मालूम पड़ता है; परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि एक ही आवरण में पाँच चैतन्य सत्ताएँ मौजूद हैं। देखा जाता है कि मनुष्य में अनेक परस्पर विरोधी तत्त्व विद्यमान रहते हैं। जब जो तत्त्व प्रबल होता है, उसके आधार पर वह अपनी दृष्टि के अनुसार पूर्ण तत्परता से काम करता है।
देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोभी है, खाने और पहनने में बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दाँतों से दबाकर पकड़ता है, परन्तु वही व्यक्ति अपने लड़के-लड़कियों की विवाह-शादी का अवसर आने पर इतनी फिजूल-खर्ची करता है कि धन को होली की तरह फूँक देता है। यह परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय-समय पर प्रकट होती हैं।
एक समय में एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु होता है, दूसरे के साथ बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है, परन्तु दूसरे समय में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जन बन जाता है कि इन दो प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है।
एक व्यक्ति बहुत संयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी-कभी उसी का वह व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है, जिसके कारण वह दुराचार में लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार अस्तिकता-नास्तिकता, सुधारकता-रूढ़िवादिता, दयालुता-निष्ठुरता, सदाचार-दुराचार, सत्य-असत्य, लोभ-त्याग, मूर्खता-बुद्धिमत्ता, निष्कपटता-वञ्चकता के परस्पर विरोधी रूप समय-समय पर मनुष्यों में प्रकट होते हैं।
इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार का है, दूसरा रूप तो उसने धोखा देने के लिए बनाया है। प्राय: बुराई के आधार पर मनुष्य का वास्तविक रूप माना जाता है और उसमें जो अच्छाई थी, उसे ढोंग कह दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है, तो भी आमतौर पर उसे सब लोग चोर मानेंगे और ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग तो उसने दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है, परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं। कोई व्यक्ति केवल मात्र आडम्बर के लिए अपना समय, श्रम, धन आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता। जब किसी दिशा में विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है, तभी उसके लिए अधिक त्याग एवं श्रम किया जाना सम्भव है।
बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का निवास होता है। एक घोंसले में कई बच्चे साथ रहते हैं, परन्तु बाहर से घोंसला एक ही दिखाई पड़ता है। गूलर के फल के भीतर भुनगे उड़ते रहते हैं, पर बाहर से उनकी प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार इस देह के अन्दर कई प्रकृतियों, स्वभावों और रुचियों के अलग-अलग व्यक्तित्व रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले कई व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि और कार्य-प्रणालियाँ अलग-अलग होती हैं। इसी तरह मनुष्य की अन्तरंग प्रवृत्तियाँ भी अनेक दिशाओं में चलती हैं।
सिर एक है, पर उसमें नाक, कान, आँख, मुख, त्वचा की पाँच इन्द्रियाँ अपना काम करती हैं। हाथ एक है, पर उसमें पाँच उँगलियाँ लगी रहती हैं, पाँचों का काम अलग-अलग है। वीणा एक है, पर उसमें कई तार होते हैं। इन तारों की सन्तुलित झंकार से ही कई स्वर लहरी बजती हैं। हाथों की पाँचों उँगलियों के सम्मिलित प्रयत्न से ही कोई काम पूरा हो सकता है। सिर में यदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ जुड़ी न हों, तो मस्तक का कोई मूल्य न रह जाए, तब खोपड़ी भी कूल्हों की तरह एक साधारण अंग मात्र रह जाएगी। विसंगतियों का एकीकरण ही जीवन है; इन भिन्नताओं के कारण ही जीवन में चेतना, क्रियाशीलता, विचारशीलता, मन्थन और प्रगति का सञ्चार होता है।
सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योगबल से जाना कि मनुष्य के शरीर में पाँच प्रकार के व्यक्तित्व, पाँच चेतना, पाँच तत्त्व विद्यमान हैं; इन्हें पाँच कोश कहते हैं। शरीर पाँच तत्त्वों का बना है। इन तत्त्वों की सूक्ष्म चेतना ही पञ्चकोश कहलाती है। यह पाँचों पृथक्-पृथक् होते हुए भी एक ही मूल केन्द्र में जुड़े हुए हैं। गायत्री के पाँचों मुखों का अलंकार इसी आधार पर है। मानव प्राणी की पाँच प्रकृतियाँ हैं, यही गायत्री के पाँच मुख हैं। यह पाँचों मुख एक ही गर्दन पर जुड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पाँचों कोश एक ही आत्मा से सम्बन्धित हैं।
महाभारत के आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य के अनुसार पाँच पाण्डव शरीरस्थ पाँच कोश ही हैं। पाँचों की एक ही स्त्री द्रौपदी है। पाँच कोशों की केन्द्र शक्ति एक आत्मा है। पाँचों पाण्डवों की अलग-अलग प्रकृति है, पाँचों कोशों की प्रवृत्ति अलग-अलग है। इस पृथकता को जब एकरूपता में, सन्तुलित समस्वरता में ढाल दिया जाता है तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है। पाँचों पाण्डवों की एक पत्नी, एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा हो जाती है, तो उनका रथ हाँकने के लिए स्वयं भगवान् को आना पड़ता है और अन्त में उन्हें ही विजयश्री मिलती है।
पाँच कोशों को मनुष्य की पञ्चधा प्रकृति कहते हैं— १-शरीराध्यास, २-गुण, ३-विचार, ४-अनुभव, ५-सत्। इन पाँच चेतनाओं को ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोश कहा जाता है। यही गायत्री के पाँच मुख हैं।
साधारणतया इन पाँचों में एकस्वरता नहीं होती। कोई किधर को चलता है, कोई किधर को। स्वास्थ्य, योग्यता, बुद्धि, रुचि और लक्ष्य में एकता न होने के कारण मनुष्य ऐसे विलक्षण कार्य करता रहता है जो किसी एक दिशा में उसे नहीं चलने देते। किसी रथ में पाँच घोड़े जुते हों, वे पाँच अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छित दिशा में रथ को खींचें, तो उस रथ की बड़ी दुर्दशा होगी। कभी वह एक फर्लांग पूर्व को चलेगा तो कभी एक मील उत्तर को खींचेगा। कोई घोड़ा पश्चिम को घसीटेगा तो कोई दक्षिण को खींचेगा। इस प्रकार रथ किसी निश्चित लक्ष्य पर न पहुँच सकेगा, घोड़ों की शक्तियाँ आपस में एक-दूसरे के प्रयत्न को रोकने में खर्च होती रहेंगी और इस खींचातानी में रथ बेतरह टूटता रहेगा।
यदि घोड़े एक निर्धारित दिशा में चलते, सबकी शक्ति मिलकर एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी से, बड़ी आसानी से वह रथ निर्दिष्ट स्थान तक पहुँच जाता। वीणा के तार बिखरे हुए हों तो उसको बजाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पर यदि वे एक स्वर-केन्द्र पर मिला लिए जाएँ और निर्धारित लहरी में उन्हें बजाया जाए तो हृदय को प्रफुल्लित करने वाला मधुर संगीत निकलेगा। जीवन में पारस्परिक विरोधी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, मान्यताएँ इस प्रकार क्रियाशील रहती हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही देह में पाँच आदमी बैठे हैं और पाँचों अपनी-अपनी मर्जी चला रहे हैं। जब जिसकी बन जाती है, तब वह अपनी ढपली पर अपना राग बजाता है।
अध्यात्मविद्या के ज्ञाताओं ने इस पृथकता को, विसंगति को एक स्थान पर केन्द्रित करने, एकसूत्र से सम्बन्धित करने के लिए पञ्चकोशों का, पञ्चमुखी गायत्री साधना का सम्विधान प्रस्तुत किया है। गायत्री के चित्र में पाँच मुख दिए गए हैं। इन पाँचों की दिशाएँ, आकृतियाँ, चेष्टाएँ देखने में अलग मालूम पड़ती हैं, परन्तु वह एक ही मूल केंद्र से सम्बद्ध होने के कारण एकस्वरता धारण किए हुए हैं। यही आदर्श गायत्री-साधक का होना चाहिए। उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, विचारधारा, अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निर्धारित लक्ष्य से संलग्न रहनी चाहिए। पाण्डव पाँच होते हुए भी एक थे। एक ही ‘पाण्डव’ शब्द कह देने से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पाँचों का बोध हो जाता है। ऐसी ही एकता हमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए।
डॉक्टर जानते हैं कि रक्त में विजातीय पदार्थों का प्रवेश हो जाए तो अनेक रोग घेर लेते हैं। ओझा लोग जानते हैं कि देह में भूत घुस जाए, एक शरीर में दो सत्ताएँ प्रवेश कर जाएँ, तो मनुष्य रोगी या उन्मादग्रस्त हो जाता है। घर में विरोधी स्वभाव की बहुएँ आ जाएँ तो परिवार में भारी क्लेश और कलह उत्पन्न हो जाता है। जब तक परस्पर विरोधी तत्त्व मनोभूमि में काम करते रहेंगे, उनकी दिशाएँ पृथक्-पृथक् रहेंगी, तब तक कोई व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता, उसके अन्त:स्थल में घोर अशान्ति घुसी रहेगी। आमतौर से लोग इसी अशान्ति में ग्रसित रहते हैं और पर्याप्त साधन सम्पन्न होते हुए भी मनुष्य जन्म जैसे अमूल्य सौभाग्य से कुछ लाभ नहीं उठा पाते। आन्तरिक विरोधों से उत्पन्न हुई गुत्थियाँ भी उनके लिए एक समस्या बन जाती हैं और मृत्यु समय तक सुलझ नहीं पातीं।
गायत्री की पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य आन्तरिक विरोधों को मिटाकर उनमें समस्वरता की स्थापना करना है। अन्तर में सत्-असत् की रस्साकशी होती है, देवासुर संग्राम, राम-रावण युद्ध, महाभारत होता रहता है। यह कलह तभी शान्त हो सकता है, जब एक पक्ष अशक्त हो जाय। असुर का, असत् का पक्ष ग्रहण करके यदि सत् को पूर्णतया कुचलने का प्रयत्न किया जाए तो वह सम्भव भी नहीं, क्योंकि असुरता स्वयं एक विपत्ति होने के कारण अपने आप अनेक संकट उत्पन्न कर लेती है। दूसरे सत् की स्थिति आत्मा में इतनी सुदृढ़ है कि उसे पूर्णतया कुचलना सम्भव नहीं है। इसलिए आन्तरिक संघर्षों की समाप्ति का एक ही उपाय है—सत् का समर्थन एवं पोषण करके उसे इतना प्रबल कर लिया जाय कि असत् को उससे संघर्ष का साहस ही न हो। लड़ाकू बकरा जब अपने सामने सिंह को खड़ा देखेगा, तो उसे लड़ने की हिम्मत न होगी। आसुरी तत्त्व तभी तक प्रबल रहते हैं, जब तक दैवी तत्त्व कमजोर होते हैं। जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लिया जाता है, तो फिर असुरता अपने हथियार डाल देती है और शान्ति का शासन स्थापित हो जाता है।
पञ्चकोशों की जो साधनाएँ पीछे बताई गई हैं, वे मनुष्य की पाँच महाशक्तियों को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोकती हैं, उन्हें नियन्त्रण में लाकर उपयोगी दिशा में लगाती हैं। सर्कस वाले खूँखार शेर-चीतों को जंगल में से पकड़ लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते हैं कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाना तो दूर, उलटे उन साधने वालों को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं। पाँच कोश पाँच शेर हैं। इन्हें साधने के लिए सरकस वालों की तरह गायत्री साधकों को भी अटूट साहस, अविचल धैर्य एवं सतत प्रयत्नशीलता को अपनाना होता है। इस साधना का आरम्भ काफी कठिनाइयों और निराशाओं से भरा हुआ होता है, परन्तु धीरे-धीरे सफलता मिलने लगती है और गायत्री साधक जब इन पाँच महा सिंहों को, पञ्चकोशों को वश में कर लेता है, तो उसे अनन्त ऐश्वर्य एवं अक्षय कीर्ति का लाभ होता है। सरकस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक सिंहों की महत्ता अनेक गुनी है, इसलिए इनके सध जाने पर सरकस वालों की अपेक्षा लाभ भी असंख्य गुने हैं। कायर इस साधना की कल्पना मात्र से डर जाते हैं, पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ परम पुरुषार्थ ही आनन्ददायक होता है।
कोशों के असन्तुलित, अविकसित, अनियन्त्रित रहने से मानव अन्त:करण की विषम स्थिति रहती है। उसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएँ, भावनाएँ और रुचियाँ उभरती एवं दबती रहती हैं। गायत्री साधना से इनमें एकता उत्पन्न होती है और अन्तर के समस्त संकल्प-विकल्पों की उधेड़बुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित गतिशीलता का आविर्भाव होता है। यह व्यवस्थित गतिशीलता जिस दिशा में भी चलेगी, उसी दिशा में आशाजनक सफलता मिलेगी।
योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्पवृक्ष है जिसके कारण वे सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, आवश्यक, लाभदायक एवं आनन्दवर्द्धक हैं। पाँच व्यक्तियों को एक ही व्यक्तित्व से सुसंयुक्त कर देना एक ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा अपनी शक्ति पाँच गुनी हो जाती है। चूँकि यह केन्द्रीकरण सतोगुण के आधार पर किया जाता है, इसलिए सात्त्विक आत्मबल की प्रचण्ड अभिवृद्धि से पञ्चमुखी गायत्री साधना का साधक महामानव, महापुरुष, महाआत्मा बन जाता है।
कीट-पतंगों की तरह सभी जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की तुच्छ क्रियाओं में संलग्न रहकर साँसें पूरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस रीति से तो पशु-पक्षी भी जी लेते हैं। बल्कि इस दृष्टि से अन्य जीव, मनुष्य से कहीं अच्छे जीते हैं। उन्हें ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, छल, दम्भ, काम, क्रोध, कुढ़न, असन्तोष, शोक, वियोग, चिन्ता आदि की आन्तरिक ग्रन्थियों में हर घड़ी झुलसते रहना नहीं पड़ता। वे अनेक प्रकार के पापों की गठरी अपने ऊपर जमा नहीं करते। मनुष्य इन सब बातों में अन्य जीव-जन्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में रहता है। मरते-मरते अन्य जीव-जन्तु अपने मृत शरीर से दूसरों का कुछ भला कर जाते हैं, पर मनुष्य वह भी नहीं कर पाता।
मानव जीवन की जो प्रशंसा और महत्ता है, उसकी आत्मिक विशेषताओं के कारण है। यदि ये विशेषताएँ अपने स्वस्थ रूप में विकसित हों, तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। योग-साधना का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अद्भुत शक्तियाँ छिपी हैं, उनको योग द्वारा इतनी उन्नत दशा तक पहुँचाया जाता है कि मनुष्य में देवत्व की झाँकी होने लगे।
भारतीय जीवन की आदिकाल से यह विशेषता रही है कि उसमें उद्देश्यमय, आदर्शयुक्त, परिमार्जित जीवन को ही प्रधानता दी गई है। इस देश में उस शक्ति को मनुष्य माना जाता रहा है, जो उद्देश्यमय आदर्श जीवन जीता रहा है। अज्ञान, आसक्ति और अभाव से संघर्ष करने का व्रत लेने वाले ही द्विज कहे जाते हैं। जो द्विज नहीं है, अर्थात् जिसने पारमार्थिक जीवन का व्रत नहीं लिया है, उस स्वार्थी, लोभी, विषयी मनुष्य को शूद्र बताकर निन्दा की है और एक प्रकार से उसका अर्द्ध सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आज तो व्यापक रूप से शूद्रता फैली हुई है। गुण, कर्म, स्वभाव से आज चाण्डाल तत्त्व और शूद्रता का विस्तृत प्रसार हो रहा है।
भारतीय संस्कृति की यह अद्भुत महानता है कि वह अपने हर अनुयायी को यह प्रेरणा देती है कि पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों जैसा शिश्नोदरपरायण तुच्छ जीवन न जीये वरन् अपना प्रत्येक क्षण महान् आदर्शों की पूर्ति में लगाए। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, शरीर-निर्वाह की जरूरतों को कम से कम रखे जिससे उनको कमाने में कम से कम समय और श्रम लगे, बचे हुए अवकाश, बुद्धिबल एवं उत्साह को महानता के सम्पादन में लगाया जा सके।
इस सांस्कृतिक प्रेरणा को ऋतम्भरा, प्रज्ञा एवं सद्बुद्धि नाम से पुकारा गया है। इसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री मन्त्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। यह सद्बुद्धि प्राचीनकाल में अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी। इसी से इस भूमि को पुण्यभूमि, तपोभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे। जीवन्मुक्त आत्माएँ ललचा-ललचाकर इस देश में अवतार लेने के लिए मुक्त-धाम से वापस लौट आती थीं। ऋतम्भरा बुद्धि ने इस देश को महान् मानवों से पाट रखा था। विद्या में, बुद्धिबल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में यह देश भरा-पूरा था। कारण कि सद्बुद्धि ने भारतवासियों की अन्त:भूमिका ऐसी परिमार्जित कर दी थी कि उससे भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों का अक्षय भण्डार उद्भव होना स्वाभाविक ही था।
सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति एवं सुख-शान्ति में रोड़ा बनती हैं। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो सुसम्पन्न बनाने के लिए आवश्यक हैं। सद्बुद्धि का एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामन्त्र के एक-एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। वह इतना उज्ज्वल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान का अन्धकार नष्ट हो जाता है। इन २४ अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान-भण्डार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अवगाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बनता है।
गायत्री के अक्षरों में ज्ञान-भण्डार तो भरा हुआ है, इसके अतिरिक्त इस महामन्त्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केन्द्रों में छिपी हुई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ जाग्रत् होती हैं, जिनके कारण दैवी वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद्बुद्धि वाले के लिए यही बड़ा कठिन है कि वह अपने आप अपने कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाए। इस कठिनाई का हल गायत्री महामन्त्र की उपासना द्वारा होता है। जो इस साधना को करते हैं, वे अनुभव करते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन:क्षेत्र में नवीन ज्ञान, नवीन प्रकाश, नवीन उत्साह आश्चर्यजनक रीति से बढ़ा रही है।
यह छोटा सा मन्त्र ‘अमर फल’ के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत का फल खाने से भी मधुर होता है और उसमें अमरता का लाभ भी होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान-विज्ञान बीज रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग से अन्त:करण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगन्ध की लोकोक्ति गायत्री के सम्बन्ध में भली प्रकार चरितार्थ होती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अत्यन्त स्वादिष्ट पौष्टिक दूध प्रचुर परिमाण में निरन्तर देती रहती है। इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक सम्पत्तियों की प्राप्ति भी होती है। इस दुहरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की अधिक महत्ता है। गायत्री की दोनों महत्ताएँ भी कामधेनु की भाँति ही हैं। इसी से उसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं।
भारतवर्ष में शिल्प, कृषि, व्यापार, विज्ञान, रसायन, शस्त्र विद्या आदि भौतिक उन्नतियों के सम्बन्ध में सदैव महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं, आज भी उनकी आवश्यकता है। पूँजी, कुशलता, श्रम एवं सहयोग के आधार पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए और यथासम्भव उन्हें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए भौतिक साधन-सामग्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है। भूखा आदमी न ईमानदार रह सकता है और न स्वस्थ चित्त। इसलिए जीवनयात्रा की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए भौतिक सम्पत्तियों का उपार्जन आवश्यक है, पर यह ध्यान रखने की बात है कि यदि भौतिक उन्नति पर ही एकमात्र ध्यान रखा गया और सम्पत्ति के ऊपर से आत्मिक नियन्त्रण उठा दिया गया, तो जो कुछ सांसारिक उन्नति होगी, वह केवल मनुष्य की आपत्तियाँ बढ़ाने का कारण बनेगी।
इन दिनों विज्ञान का बड़ा जोर है, सुविधाओं के साधन नित नए निकलते जा रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य विलासी, आलसी, दुर्बल, रोगी, कायर और अल्पजीवी होता चला जा रहा है। जिन देशों ने अपनी शक्ति बढ़ाई है, वे छोटे देशों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों का परिणाम यह है कि एटम बम, हाइड्रोजन बम संसार में प्रलय उपस्थित करने के लिए तैयार हैं। साधारण लोगों पर दृष्टि डालिए तो उनका भी यही हाल है। भौतिक शक्ति पाकर लोग अपना और दूसरों का विनाश ही करते हैं। वकीलों की विद्या से किसका क्या हित है? ज्यादा कमाने वाले मजदूर शराब और ताड़ी में अपनी कमाई फूँक देते हैं। साहसी स्वभाव और बलवान् शरीर वाले गुण्डा, डाकू, अत्याचारी बनने में अपना गौरव देखते हैं। देहातों में आजकल अन्न की महँगाई से किसानों की आर्थिक दशा थोड़ी सुधरी है, तो फौजदारी, मुकदमेबाजी, विवाह-शादियों आदि बातों में फिजूलखर्ची की बेतरह बाढ़ आ गई है। यह निश्चित है कि यदि भौतिक उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश न होगा, तो वह भस्मासुर के वरदान की तरह अपना ही सर्वनाश करने वाली सिद्ध होगी। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ-साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए। सुन्दर बहुमूल्य वस्त्राभूषण तभी शोभा पाते हैं, जब पहनने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो। मरणासन्न अस्थिपंजर रोगी को यदि रेशमी कपड़ों से और जेवर से लाद दिया जाए, तो उसकी शोभा तो कुछ न बढ़ेगी, उलटे उसकी असुविधा बढ़ जाएगी। आत्मिक उन्नति के बिना भौतिक सम्पदाओं की बढ़ोत्तरी से मनुष्य की अहंकारिता, ईर्ष्या, विलासिता, कुरुचि, चिन्ता, कुढ़न, शत्रुता आदि कष्टकारक बुराइयाँ भी बढ़ जाती हैं।
गायत्री आत्मोन्नति का, आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सांसारिक सम्पत्तियाँ उपार्जन करना जिस प्रकार आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार गायत्री-साधना द्वारा आत्मिक पूँजी बढ़ाने का प्रयत्न भी निरन्तर जारी रहना चाहिए। दोनों दिशाओं में साथ-साथ सन्तुलित विकास होगा तो स्वस्थ उन्नति होगी, किन्तु यदि केवल धन या भोग के सञ्चय में ही लगा रहा गया, तो निश्चित है कि वह कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकट्ठी भले ही दीखे, पर उसमें वास्तविक सुख की उपलब्धि तनिक भी न हो सकेगी। जो सांसारिक वस्तुओं का समुचित लाभ उठाना चाहता हो, उसे चाहिए कि आत्मोन्नति के लिए उतना ही प्रयत्न करे।
आँखों के बिना सुन्दर दृश्य देखने का लाभ नहीं मिल सकता, कान बहरे हों तो मधुर संगीत का रसास्वादन सम्भव नहीं। आत्मिक शक्ति न हो ,तो सांसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लाभ नहीं उठाया जा सकता है। सुन्दर दृश्य और तीव्र नेत्र ज्योति के संयोग से ही चित्त प्रसन्न होता है। भौतिक और आत्मिक उन्नति का समन्वय ही जीवन में सुस्थिर शान्ति की स्थापना कर सकता है। हम धन कमाएँ, विद्या पढ़ें और उन्नति करें, पर यह न भूलें कि इसका वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा, जब आत्मोन्नति के लिए भी समुचित साधना की जा रही हो।
१-स्वास्थ्य, २-धन, ३-विद्या, ४-चतुरता, ५-सहयोग, यह पाँच सम्पत्तियाँ इस संसार में होती हैं। इन्हीं पाँच के अन्तर्गत समस्त प्रकार के वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार पाँच कोशों की परिमार्जित स्थिति ही पाँच आध्यात्मिक सम्पदाएँ हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय—यह पाँच कोश आध्यात्मिक शक्तियों के पाँच भण्डार हैं। इन कोशों पर जो अधिकार कर लेता है, उसकी अन्त:चेतना का पञ्चीकरण हो जाता है और १-आत्मज्ञान, २-आत्मदर्शन, ३-आत्मानुभव, ४-आत्मलाभ, ५-आत्मकल्याण, यह पाँच आध्यात्मिक सम्पदाएँ प्राप्त हो जाती हैं।
गायत्री के चित्र में दस भुजाएँ दिखाई गई हैं—पाँच बायीं और पाँच दाहिनी ओर। बायीं ओर की पाँच भुजाएँ सांसारिक सम्पत्तियाँ हैं और दाहिनी ओर की भुजाएँ पाँच आत्मिक शक्तियाँ हैं। गायत्री उपासक इन दसों लाभों को प्राप्त करके रहता है।
(१) ‘आत्मज्ञान’ का अर्थ है—अपने को जान लेना, शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेना और शारीरिक लाभों को आत्मलाभ की तुलना में उतना ही महत्त्व देना जितना कि दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर हो जाता है। इन्द्रिय भोगों की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अनुचित, अनावश्यक व्यय होता है, जिससे शरीर असमय में ही दुर्बल, रोगी, कुरूप एवं जीर्ण हो जाता है। आत्मज्ञानी इन्द्रिय भोगों की उपयोगिता-अनुपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ की दृष्टि से करता है, इसलिए वह स्वभावत: संयमी रहता है और शरीर से सम्बन्ध रखने वाले दु:खों से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं कुरूपता का कष्ट उसे नहीं भोगना पड़ता। जो कष्ट उसे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं, वह भी आसानी से भुगत जाते हैं।
(२) ‘आत्मदर्शन’ का तात्पर्य है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है, तब प्रीति-प्रतीति, श्रद्धा-निष्ठा और विश्वास की भावनाएँ बढ़ती हैं। कभी भौतिकवादी, कभी अध्यात्मवादी होने की डावाँडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण, कर्म, स्वभाव प्रकट होने लगते हैं, जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित हैं। उस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका में पहुँचने पर दूसरों को जानने, समझने और उन्हें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है।
जिसे आत्मदर्शन हुआ है उसकी आत्मिक सूक्ष्मता अधिक व्यापक हो जाती है, वह संसार के सब शरीरों में अपने को समाया हुआ देखता है। जैसे अपने मनोभाव, आचरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरों के भीतर की सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती हैं। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन से काम लेने में समर्थ होते हैं, वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीरों पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है।
(३) ‘आत्मानुभव’ कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना, अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार पर ही अपनी वाणी, क्रिया, योजना, इच्छा, आकांक्षा, रुचि एवं भावना का होना। आमतौर से लोग विचार तो बहुत ऊँचे रखते हैं, पर बाह्य जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते। उनका व्यावहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है। किन्तु जिन्हें आत्मानुभव होता है, वे भीतर-बाहर एक होते हैं। उनके विचार और कार्यों में तनिक भी अन्तर नहीं होता। जो विघ्न-बाधाएँ सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ती हैं, उन्हें वे एक ठोकर से तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है।
आत्म-अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिलती है। किसका क्या भविष्य बन रहा है? भूतकाल में कौन क्या कर रहा है? किस कार्य में दैवी प्रेरणा क्या है? क्या उपद्रव और भय उत्पन्न होने वाले हैं? लोक-लोकान्तरों में क्या हो रहा है? कब, कहाँ, क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है? आदि ऐसी अदृश्य एवं अज्ञात बातें, जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते, उन्हें आत्मानुभव की भूमिका में पहुँचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है। आरम्भ में उसे अनुभव कुछ धुँधले होते हैं, पर जैसे-जैसे उनकी दिव्यदृष्टि निर्मल होती जाती है, सब कुछ चित्रवत् दिखाई देने लगता है।
(४) ‘आत्मलाभ’ का अभिप्राय है-अपने में पूर्ण आत्मतत्त्व की प्रतिष्ठा। जैसे भट्ठी में पड़ा लोहा तपकर अग्निवर्ण सा लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुँचा हुआ सिद्ध पुरुष दैवी तेजपुञ्ज से परिपूर्ण हो जाता है। वह सत् की प्रत्यक्ष मूर्ति होता है। जैसे अँगीठी के पास बैैठने से गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही महापुरुषों के आस-पास ऐसा सतोगुणी वातावरण छाया रहता है, जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शान्ति अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में ग्रीष्म की धूप से तपे हुए लोगों को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेक दु:खियों को शान्ति प्रदान करते रहते हैं।
आत्मलाभ के साथ-साथ आत्मा की-परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों से सम्बन्ध हो जाता है। परमात्मा की एक-एक शक्ति का प्रतीक एक-एक देवता है। यह देवता अनेक ऋद्धि-सिद्धियों का अधिपति है। ये देवता जैसे विश्व-ब्रह्माण्ड में व्यापक हैं, वैसे ही मानव शरीर में भी हैं। विश्व-ब्रह्माण्ड का ही एक छोटा सा रूप यह पिण्ड देह है। इस पिण्ड देह में जो दैवी शक्तियों के गुह्य संस्थान हैं, वे आत्मलाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वह उन दैवी शक्तियों से इच्छानुसार कार्य ले सकता है।
(५) ‘आत्मकल्याण’ का अर्थ है—जीवन-मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अक्षय आनन्द, ब्रह्मनिर्वाण, स्थित-प्रज्ञावस्था, परमहंस -गति, ईश्वर -प्राप्ति। इस पञ्चम भूमिका में पहुँचा हुआ साधक ब्राह्मीभूत होता है। इसी पञ्चम भूमिका में पहुँची हुई आत्माएँ ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती हैं। उन्हें देवदूत, अवतार, पैगम्बर, युगनिर्माता, प्रकाश स्तम्भ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज ऐसी नहीं, जो उन्हें अप्राप्य हो। वे अक्षय आनन्द के स्वामी होते हैं। ब्रह्मानन्द, परमानन्द एवं आत्मानन्द से बड़ा और कोई सुख इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में सम्भव नहीं; यही सर्वोच्च लाभ आत्मकल्याण की भूमिका में पहुँचे हुए को प्राप्त हो जाता है।
दशभुजी गायत्री की पाँच भुजा सांसारिक हैं, पाँच आत्मिक। आत्मिक भुजाएँ, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मानुभव, आत्मलाभ और आत्मकल्याण हैं। यह दैवी सम्पदाएँ जिनके पास हैं, उनके वैभव की तुलना कुबेर से भी नहीं हो सकती। गायत्री का उपासक आत्मिक दृष्टि से इतना सुसम्पन्न और परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी तुलना किन्हीं भी सांसारिक सम्पदाओं से नहीं की जा सकती। ये पाँचों भूमिकाएँ, सिद्धियाँ, पञ्चकोशों से सम्बन्धित हैं। एक-एक कोश की साधना एक-एक भूमिका में प्रवेश कराती जाती है। अन्नमय कोश का साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। प्राणमय कोश की साधना से आत्मदर्शन होता है, मनोमय कोश के साथ आत्मानुभव होता है, विज्ञानमय कोश से आत्मलाभ का सम्बन्ध है और आनन्दमय कोश में आत्मकल्याण सन्निहित है।
दशभुजी गायत्री की पाँच भुजाएँ सूक्ष्म और पाँच स्थूल हैं। निष्काम उपासना करने वाले माता के सूक्ष्म हाथों से आशीर्वाद पाते हैं और सकाम उपासकों को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने माता की कृपा से सांसारिक सम्पत्तियाँ प्राप्त की हैं और अपनी दुर्गम कठिनाइयों से त्राण पाया है। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग, ये पाँच सांसारिक सम्पत्तियाँ पञ्चमुखी माता की स्थूल भुजाओं से मिलती हैं।
ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं, जिनमें लोगों ने साधारण गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलताएँ प्राप्त की हैं। जिनके घर में रोग घुस रहा था, बीमारी की पीड़ा सहते-सहते और डॉक्टरों का घर भरते-भरते जो कातर हो रहे थे, उन्होंने रोगमुक्ति के वरदान पाए। क्षय सरीखे प्राणघातक रोगों की मृत्युशय्या पर से उठकर खड़े हो गए। कइयों को जन्मजात पैतृक रोगों तक से छुटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति अच्छी जीविका के अधिकारी बन गए। साधनहीन और अविकसित लोग चतुर, बुद्धिमान्, कलाकार, शिल्पी, गुणवान्, प्रतिभावान्, सर्वप्रिय नेता और यशस्वी बन गए। जिनको सब ओर से तिरस्कार, अपमान, द्वेष, संघर्ष और असहयोग ही मिलता था, उनको घर-बाहर सर्वत्र प्रेम, सहयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा।
ऐसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं परिचित हैं। मुकदमा, आक्रमण, बन्धन, भय, आशंका, विरोध, परीक्षा, बीमारी, दरिद्रता, भूत-बाधा, सन्तति-कष्ट, व्यसन, दुर्गुण आदि कुचक्रों के त्रासदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यक्तियों ने सन्तोष की साँस ली है। कष्टकर वर्तमान और भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो रहे थे, उन्होंने जब गायत्री का आश्रय लिया तो तत्क्षण उन्हें धैर्य, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ। यह ठीक है कि कोई देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया, पर यह भी सत्य है कि उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई, जिससे झट बिगड़ा काम बन गया और पर्वत-सी भारी कठिनाई राई की तरह छोटी होकर हल हो गई। जिस आपत्ति में यह लगता था कि न जाने इसके कारण हम पर क्या बीतेगी, वह सब आशंकाएँ काई की तरह फट गईं और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं।
स्वास्थ्य और धन की ही भाँति दशभुजी गायत्री की तीसरी स्थूल भुजा का प्रसाद ‘विद्या’ के रूप में मिलता है। मन्दबुद्धि, मूढ़मगज, भुलक्कड़, मूर्ख, अदूरदर्शी, सिड़ी, सनकी एवं अर्द्धविक्षिप्त मनुष्यों को बुद्धिमान्, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान् बनते देखा गया है। जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई यह भविष्यवाणी करता था कि अपना पेट भी न भर सकेंगे, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गए, लोग उनकी सलाह लेकर काम करने में अपनी भलाई समझने लगे।
जिनकी पढ़ाई में रुचि न थी, वे पुस्तकों के कीड़े हो गए। हर साल फेल होने वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से ऐसे तीव्र बुद्धि के हुए कि सदैव अच्छे नम्बरों से उन्हें सफलता मिलती गई। अनेक उलझनें, कार्यव्यस्तता एवं अवकाश का अभाव रहने पर भी कितने ही साधनहीन व्यक्ति विद्वान् बने हैं। मस्तिष्क से काम लेने वाले कितने ही बुद्धिजीवी मनुष्य ऐसे हैं, जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यन्त प्रखर बनाया है और फलस्वरूप वे उज्ज्वल नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए हैं। अपने बुद्धिबल से उन्होंने आशाजनक सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति और सम्पदा उपार्जित की है।
विकृत मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजा के प्रसाद से स्वस्थ मनोभूमि प्राप्त करते हैं। भूतोन्माद, प्रेतबाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत शक्ति गायत्री उपासना में है। हजार ओझा, सयाने और तान्त्रिक तराजू के एक पलड़े में रखे जाएँ और एक गायत्री उपासक एक ओर रखा जाए, तो निश्चित रूप से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध होगी।
चातुर्यपूर्ण कामों का आरम्भ करते समय शारदा का, सरस्वती का आह्वान, वन्दन और पूजन करने की प्रथा है। कारण यही है कि बुद्धि तत्त्व में माता की कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है, जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयंगम हो जाती हैं। चित्रकला, संगीत, कविता, सम्भाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, शिक्षण, नेतृत्व, अन्वेषण, परीक्षण, निर्णय, दलाली, प्रचार, व्यवसाय, खेल, प्रतिद्वन्द्विता कूटनीति आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं, जिनमें विशेष सफलता वही पा सकता है जिसकी बुद्धि में सूक्ष्मता हो। मोटी अक्ल से इस प्रकार के कर्मों में लाभ नहीं होता। कुशाग्र, सूक्ष्मवेधी बुद्धि-चातुर्य गायत्री माता के पुण्य-प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्यों को आरंभ करते हुए शारदा-वन्दना करते हैं।
गायत्री की स्थूल पाँच भुजाओं में पाँचवीं भुजा का प्रसाद सहयोग है। यह जिसे मिलता है, वह स्वयं विनम्र, मधुरभाषी, प्रसन्नचित्त, हँसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहृदय, सेवाभावी, निरहंकारी बन जाता है। ये विशेषताएँ उनमें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, फलस्वरूप उनके संपर्क में जो भी कोई आता है, वह उनका बेपैसे का गुलाम बन जाता है। ऐसे स्वभाव के मनुष्य के स्त्री, पुरुष, पुत्र, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ सभी अनुकूल, सहायक और प्रशंसक रहते हैं। घर में उसका मान-सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। घर में हों, बाहर बाजार में, मित्रों में, परिचितों में, सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति कहीं भी मित्रविहीन नहीं रहते। वे जहाँ भी रहते हैं, वहीं उन्हें प्रेमी, प्रशंसक, मित्र, सहायक-सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं।
दाहिनी और बाईं, सूक्ष्म और स्थूल गायत्री की दस भुजाएँ साधक को प्राप्त होने वाली पाँच आत्मिक और पाँच भौतिक सिद्धियाँ हैं। ये दस सिद्धियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा यही जीवन, यही लोक स्वर्गीय सुख से ओत-प्रोत हो जाता है। यह जीवन अगले जीवन की पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज संतुष्ट है तो कल भी उसे संतोष ही उपलब्ध होगा, यदि आज उसे कल्याण का अनुभव होता है तो कल कल भी कल्याण ही होगा। सत्पुरुष अक्सर दुस्साहसपूर्ण और वर्तमान वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं, इसलिए बाह्य दृष्टि से उन्हें कुछ असुविधाएँ दिखाएँ देती हैं। परन्तु उनकी आन्तरिक स्थिति पूर्ण प्रसन्न और सन्तुष्ट होती है। ऐसी दशा में यह भी निश्चित है कि उनका अगला जीवन भी पूर्णतया प्रसन्नता एवं संतोष की भूमिका में और भी अधिक विकसित होगा और आज की बाह्य कठिनाइयाँ भी कल तक स्थिर न रहेंगी।
क्या योग साधना के लिए घर-गृहस्थ छोड़कर साधु बनना, कपड़े रँगना, यत्र-तत्र भ्रमण करते रहना आवश्यक है? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पूर्वकाल के योगियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्राचीनकाल में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे, यह मान्यता ठीक नहीं। यह ठीक है कि ऋषि-मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे, यह बात भी बिलकुल ठीक है। स्त्री-बच्चों के साथ होने से उन्हें तपश्चर्या एवं आत्मोन्नति में सहायता मिलती थी।
इतिहास-पुराणों में पग-पग पर इस बात की साक्षी मिलती है कि भारतीय महर्षिगण योगी, यती, साधु, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रचयिता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेता आदि विविध रूपों में अपना जीवन यापन करते थे और इन महान् कार्यों में स्त्री-बच्चों को भी अपना भागीदार बनाते थे।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विवाहित थे। ब्रह्मा की गायत्री और सावित्री दो स्त्रियाँ थीं। विष्णु की तुलसी और लक्ष्मी दो पत्नी हैं। सती के मरने के बाद महादेव जी का दूसरा विवाह पार्वती से हुआ था। व्यास, अत्रि, गौतम, वसिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, च्यवन आदि सभी ऋषि गृहस्थ ही थे। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ गार्गी और मैत्रेयी थीं। अत्रि की पत्नी अनसूया अपने समय की प्रमुख ब्रह्मवादिनी थी। ऐसे प्रमाणों से इतिहास-पुराणों का पन्ना-पन्ना भरा पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में योगी लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते थे।
उस समय की परिस्थितियाँ, प्रथाएँ, सुविधाएँ तथा सादगी की पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्त्विक जीवन बिताते थे। वेश बनाने या घर छोड़ने की उनकी कोई योजना न थी। लकड़ी की खड़ाऊँ, तुम्बी का जलपात्र उनकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे। उस समय आबादी कम और वन अधिक थे। आसानी से बन सकने वाली झोंपड़ी, छोटे-छोटे ग्राम उस समय की साधारण परिपाटी थी। पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में उन बातों की नकल करना कहाँ तक उचित है, यह पाठक स्वयं सोच सकते हैं।
उस समय दूध पीकर फल खाकर रहने वाले लोग त्यागी नहीं समझे जाते थे, क्योंकि विस्तृत वनों में चरने की सुविधा होने से कोई मनुष्य कितनी ही गाएँ पाल सकता था। जंगलों मे अपने आप उगे फलों को लाने में कोई बाधा न थी। पर आज तो एक गाय पालने में एक परिवार के बराबर खर्च आता है। पेट को खराब कर डालने वाले फलों को न लेकर यदि सुखाद्य फलों को लिया जाए, तो भी काफी खर्च होता है। जो बात उस समय अत्यन्त सादगी की थी, वह आज अमीरों के लिए भी दुर्लभ है।
रास्ते रोके पड़ी रहने वाली, टूटे हुए वृक्षों की सूखी लकड़ी को साफ करने तथा हिंसक जानवरों का आक्रमण रोकने के लिए दिन-रात ‘धूनी’ जलाई जाती थी। पर आज तो लकड़ी का भाव इतना अधिक है जिसे किसी भी स्थिति में वहन नहीं किया जा सकता। उस समय स्वाभाविक मृत्यु से मरते रहने वाले मृग आदि जीवों का चमड़ा चाहे जितना मिलता था। पर आज तो बिना हत्या का चमड़ा प्राप्त करना असंभव-सा लगता है। फिर एक मृगचर्म का मूल्य भी कल्पनातीत है। इतने रुपए से तो कुश के ढेरों आसन खरीदे जा सकते हैं। सर्दी-गर्मी से बचने के लिए देह पर भस्म मलने से, भभूत रमाने से काम चल जाता था। वस्त्र वहाँ जंगलों में थे नहीं। पर आज जब वस्त्रों का मिलना सुगम है, तो भभूत लगाने की क्या आवश्यकता है?
उस जमाने में पेड़ काटने, अग्नि सँभालने, जंगली पशुओं से मुकाबला करने के लिए बड़ा-सा चिमटा रखना आवश्यक था, पर आज जब कि वह तीनों ही कारण नहीं रहे, तो चिमटे का क्या प्रयोजन रह गया? पूर्वकाल में जिन बातों को सादगी एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक आवश्यक समझा जाता था, आज की परिस्थितियों में उनमें से कितनी ही बातें अनावश्यक हैं। हमने भारतवर्ष की एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार आध्यात्मिक यात्राएँ की हैं। अपने अनुभव के बल पर हम कह सकते हैं कि अब कोई वन ऐसा नहीं रहा है, जहाँ फल खाकर या अपने आप चरकर आने वाली गौओं का दूध पीकर कोई व्यक्ति गुजारा कर सके, न आज के मनुष्यों के शरीर ही ऐसे हैं कि शीत प्रधान देशों में मकान या वस्त्रों के बिना रह सकें। जो योगी-यती गंगोत्री आदि में रहते हैं, उनको भी वस्त्र, मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है।
भिक्षाजीवी होकर, दूसरों से ऋण लेकर आज की अभावग्रस्त जनता पर, अश्रद्धालु जनता पर भार बनकर ‘साधु’ वेश बना लेना, बदली हुई परिस्थितियों का विचार न करके पूर्वजों की वेशभूषा का अन्धानुकरण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। साधु हो जाने वालों को भी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है, जितना कि गृहस्थ को। ऐसी दशा में यही उचित है कि अपनी जीविका की आप व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सादा वेश में साधु जीवन व्यतीत किया जाए।
साधना मन से होती है न कि वेश से। मन तो भारी भीड़ में भी शांत रह सकता है और एकांत वन में भी विकारग्रस्त हो सकता है, फिर एकांतसेवी लोगों की इंद्रिय-विजय भी कच्ची होती है। जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलता, वह ईमानदार है। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रलोभन के वक्त वह फिसल सकता है। जिसको चोरी के सदा अवसर हैं, फिर भी अपने पर काबू रखता है, उसी को विश्वस्त, प्रमाणिक, ईमानदार कहा जाएगा। एकान्त जंगल में बैठकर, लोगों से संबंध तोड़कर कोई व्यक्ति बुराइयों से बच जाए, तो उसके संस्कार उतने सुदृढ़ नहीं हो सकते जितने कि निरन्तर बुराइयों से संघर्ष करके अपनी अच्छाई को विकसित करने वाले के होते हैं। शूर की परीक्षा युद्धभूमि में होती है। घर में बैठा हुआ तो मरीज भी तीसमारखाँ कहला सकता है।
गायत्री-साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उन्नति करने एवं कल्याण-पथ पर चलने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं कि कोई विचित्र वेश बनाया जाए, घर-द्वार छोड़कर भीख के टूँकों पर गुजारा किया जाए। कुछ विशिष्ट आत्माएँ संन्यास की अधिकारी होती हैं। वह अधिकार तब मिलता है, जब साधना पूर्ण परिपक्व होकर मनोभूमि इस योग्य हो जाती है कि वह संसार का पथ-प्रदर्शन करने के लिए परिव्राजक बने। साधारण साधकों के लिए यह मार्ग ग्रहण करना अनधिकार चेष्टा करना है।
गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, निश्चित आहार-विहार की सुविधा घर छोड़ने वाले को नहीं हो सकती। पात्र-कुपात्रों का अन्न, पेट में जाकर बुद्धि पर तरह-तरह के संस्कार डालता है, इसलिए अपने परिश्रम की कमाई हुई रोटी पर गुजारा करते हुए गृहस्थ जीवन में ही साधनाक्रम का आयोजन करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य उचित और आवश्यक है, जिससे जितना संयम हो सके उतना अच्छा है। पुरश्चरण की निश्चित अवधि में जब तक निश्चित संकल्प का जप पूरा न हो, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। परन्तु नियतकालीन निर्धारण संख्या या अवधि के विशेष पुरश्चरणों को छोड़कर, सामान्य साधनाक्रम में ब्रह्मचर्य अनिवार्य शर्त नहीं है। गृहस्थ लोग अपने साधारण एवं स्वाभाविक दाम्पत्य कर्त्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपनी साधना जारी रख सकते हैं। इससे उनके साधन में कोई बाधा न आएगी।
मन पर नियन्त्रण करने की सात्त्विकता के नियम पालन करने की सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। जहाँ पानी होगा, वहीं तो तैरना सीखा जाएगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला अच्छा तैराक किस प्रकार बन सकेगा? तैरने की अनेक शिक्षाएँ ग्रहण करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक कि वह पानी में रहकर भी न डूबने की अपनी योग्यता प्रमाणित न कर दे। गृहस्थ जीवन में अनेक अनुकूल-प्रतिकूल, भले-बुरे, हर्ष-विषाद के अवसर आते हैं, उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन के साधन से स्वभाव और संस्कारों में प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आती है।
अपने बुरे संस्कारों एवं स्वभावों से नित्य संघर्ष करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए घोर प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर प्रयत्न एवं संघर्ष को मन्थन कहते हैं। इसे ही गीता में ‘धर्मयुद्ध’ या ‘कर्मयोग’ कहा है। अर्जुन चाहता है-हमारा अज्ञानग्रस्त मन कहता है कि इस झंझट से दूर रहकर, एकान्तवासी बनकर सफलता का कोई दूसरा मार्ग मिल जाए। वह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि संघर्ष सदा ही कष्टसाध्य होता है। मनुष्य की कायर प्रकृति सदा उससे बचना चाहती है। कायर सिपाही सदा ही लड़ाई के मोर्चे से भाग खड़े होने की योजना बनाते हैं। इसी प्रकार अपने स्वभाव की, परिवार की, समाज की, देश-काल की परिस्थितियों से खीजकर कई आदमी निराश होकर बुराइयों को आत्मसमर्पण ही कर देते हैं।
इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान् ने बुरी तरह लताड़ा था और उसके तर्कों में झाँकती हुई कायरता का पर्दाफाश कर दिया था। भगवान् ने कहा—‘‘बिना लड़े कल्याण नहीं, सफलता-असफलता की बात को मन से हटाकर लड़ने को अपने कर्त्तव्य मानकर तू लड़।’’ साधकों के लिए भी यही मार्ग है। विपरीत परिस्थितियों से उन्हें निरन्तर अति उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इतना प्रयत्न करने पर भी कम सफलता मिली, यह सोचना धर्मयुद्ध के विज्ञान के विपरीत है। संघर्ष एक साधना है। उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। मन्थन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। साधन-समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों न हो, प्रगति चाहे कितनी मन्द क्यों न हो, पर यह ध्रुव निश्चय है कि यदि साधक की यात्रा उसी दशा में जारी है, तो वह आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके रहेगा।
देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोभी है, खाने और पहनने में बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दाँतों से दबाकर पकड़ता है, परन्तु वही व्यक्ति अपने लड़के-लड़कियों की विवाह-शादी का अवसर आने पर इतनी फिजूल-खर्ची करता है कि धन को होली की तरह फूँक देता है। यह परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय-समय पर प्रकट होती हैं।
एक समय में एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु होता है, दूसरे के साथ बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है, परन्तु दूसरे समय में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जन बन जाता है कि इन दो प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है।
एक व्यक्ति बहुत संयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी-कभी उसी का वह व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है, जिसके कारण वह दुराचार में लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार अस्तिकता-नास्तिकता, सुधारकता-रूढ़िवादिता, दयालुता-निष्ठुरता, सदाचार-दुराचार, सत्य-असत्य, लोभ-त्याग, मूर्खता-बुद्धिमत्ता, निष्कपटता-वञ्चकता के परस्पर विरोधी रूप समय-समय पर मनुष्यों में प्रकट होते हैं।
इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार का है, दूसरा रूप तो उसने धोखा देने के लिए बनाया है। प्राय: बुराई के आधार पर मनुष्य का वास्तविक रूप माना जाता है और उसमें जो अच्छाई थी, उसे ढोंग कह दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है, तो भी आमतौर पर उसे सब लोग चोर मानेंगे और ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग तो उसने दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है, परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं। कोई व्यक्ति केवल मात्र आडम्बर के लिए अपना समय, श्रम, धन आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता। जब किसी दिशा में विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है, तभी उसके लिए अधिक त्याग एवं श्रम किया जाना सम्भव है।
बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का निवास होता है। एक घोंसले में कई बच्चे साथ रहते हैं, परन्तु बाहर से घोंसला एक ही दिखाई पड़ता है। गूलर के फल के भीतर भुनगे उड़ते रहते हैं, पर बाहर से उनकी प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार इस देह के अन्दर कई प्रकृतियों, स्वभावों और रुचियों के अलग-अलग व्यक्तित्व रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले कई व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि और कार्य-प्रणालियाँ अलग-अलग होती हैं। इसी तरह मनुष्य की अन्तरंग प्रवृत्तियाँ भी अनेक दिशाओं में चलती हैं।
सिर एक है, पर उसमें नाक, कान, आँख, मुख, त्वचा की पाँच इन्द्रियाँ अपना काम करती हैं। हाथ एक है, पर उसमें पाँच उँगलियाँ लगी रहती हैं, पाँचों का काम अलग-अलग है। वीणा एक है, पर उसमें कई तार होते हैं। इन तारों की सन्तुलित झंकार से ही कई स्वर लहरी बजती हैं। हाथों की पाँचों उँगलियों के सम्मिलित प्रयत्न से ही कोई काम पूरा हो सकता है। सिर में यदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ जुड़ी न हों, तो मस्तक का कोई मूल्य न रह जाए, तब खोपड़ी भी कूल्हों की तरह एक साधारण अंग मात्र रह जाएगी। विसंगतियों का एकीकरण ही जीवन है; इन भिन्नताओं के कारण ही जीवन में चेतना, क्रियाशीलता, विचारशीलता, मन्थन और प्रगति का सञ्चार होता है।
सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योगबल से जाना कि मनुष्य के शरीर में पाँच प्रकार के व्यक्तित्व, पाँच चेतना, पाँच तत्त्व विद्यमान हैं; इन्हें पाँच कोश कहते हैं। शरीर पाँच तत्त्वों का बना है। इन तत्त्वों की सूक्ष्म चेतना ही पञ्चकोश कहलाती है। यह पाँचों पृथक्-पृथक् होते हुए भी एक ही मूल केन्द्र में जुड़े हुए हैं। गायत्री के पाँचों मुखों का अलंकार इसी आधार पर है। मानव प्राणी की पाँच प्रकृतियाँ हैं, यही गायत्री के पाँच मुख हैं। यह पाँचों मुख एक ही गर्दन पर जुड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पाँचों कोश एक ही आत्मा से सम्बन्धित हैं।
महाभारत के आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य के अनुसार पाँच पाण्डव शरीरस्थ पाँच कोश ही हैं। पाँचों की एक ही स्त्री द्रौपदी है। पाँच कोशों की केन्द्र शक्ति एक आत्मा है। पाँचों पाण्डवों की अलग-अलग प्रकृति है, पाँचों कोशों की प्रवृत्ति अलग-अलग है। इस पृथकता को जब एकरूपता में, सन्तुलित समस्वरता में ढाल दिया जाता है तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है। पाँचों पाण्डवों की एक पत्नी, एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा हो जाती है, तो उनका रथ हाँकने के लिए स्वयं भगवान् को आना पड़ता है और अन्त में उन्हें ही विजयश्री मिलती है।
पाँच कोशों को मनुष्य की पञ्चधा प्रकृति कहते हैं— १-शरीराध्यास, २-गुण, ३-विचार, ४-अनुभव, ५-सत्। इन पाँच चेतनाओं को ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोश कहा जाता है। यही गायत्री के पाँच मुख हैं।
साधारणतया इन पाँचों में एकस्वरता नहीं होती। कोई किधर को चलता है, कोई किधर को। स्वास्थ्य, योग्यता, बुद्धि, रुचि और लक्ष्य में एकता न होने के कारण मनुष्य ऐसे विलक्षण कार्य करता रहता है जो किसी एक दिशा में उसे नहीं चलने देते। किसी रथ में पाँच घोड़े जुते हों, वे पाँच अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छित दिशा में रथ को खींचें, तो उस रथ की बड़ी दुर्दशा होगी। कभी वह एक फर्लांग पूर्व को चलेगा तो कभी एक मील उत्तर को खींचेगा। कोई घोड़ा पश्चिम को घसीटेगा तो कोई दक्षिण को खींचेगा। इस प्रकार रथ किसी निश्चित लक्ष्य पर न पहुँच सकेगा, घोड़ों की शक्तियाँ आपस में एक-दूसरे के प्रयत्न को रोकने में खर्च होती रहेंगी और इस खींचातानी में रथ बेतरह टूटता रहेगा।
यदि घोड़े एक निर्धारित दिशा में चलते, सबकी शक्ति मिलकर एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी से, बड़ी आसानी से वह रथ निर्दिष्ट स्थान तक पहुँच जाता। वीणा के तार बिखरे हुए हों तो उसको बजाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पर यदि वे एक स्वर-केन्द्र पर मिला लिए जाएँ और निर्धारित लहरी में उन्हें बजाया जाए तो हृदय को प्रफुल्लित करने वाला मधुर संगीत निकलेगा। जीवन में पारस्परिक विरोधी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, मान्यताएँ इस प्रकार क्रियाशील रहती हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही देह में पाँच आदमी बैठे हैं और पाँचों अपनी-अपनी मर्जी चला रहे हैं। जब जिसकी बन जाती है, तब वह अपनी ढपली पर अपना राग बजाता है।
अध्यात्मविद्या के ज्ञाताओं ने इस पृथकता को, विसंगति को एक स्थान पर केन्द्रित करने, एकसूत्र से सम्बन्धित करने के लिए पञ्चकोशों का, पञ्चमुखी गायत्री साधना का सम्विधान प्रस्तुत किया है। गायत्री के चित्र में पाँच मुख दिए गए हैं। इन पाँचों की दिशाएँ, आकृतियाँ, चेष्टाएँ देखने में अलग मालूम पड़ती हैं, परन्तु वह एक ही मूल केंद्र से सम्बद्ध होने के कारण एकस्वरता धारण किए हुए हैं। यही आदर्श गायत्री-साधक का होना चाहिए। उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, विचारधारा, अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निर्धारित लक्ष्य से संलग्न रहनी चाहिए। पाण्डव पाँच होते हुए भी एक थे। एक ही ‘पाण्डव’ शब्द कह देने से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पाँचों का बोध हो जाता है। ऐसी ही एकता हमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए।
डॉक्टर जानते हैं कि रक्त में विजातीय पदार्थों का प्रवेश हो जाए तो अनेक रोग घेर लेते हैं। ओझा लोग जानते हैं कि देह में भूत घुस जाए, एक शरीर में दो सत्ताएँ प्रवेश कर जाएँ, तो मनुष्य रोगी या उन्मादग्रस्त हो जाता है। घर में विरोधी स्वभाव की बहुएँ आ जाएँ तो परिवार में भारी क्लेश और कलह उत्पन्न हो जाता है। जब तक परस्पर विरोधी तत्त्व मनोभूमि में काम करते रहेंगे, उनकी दिशाएँ पृथक्-पृथक् रहेंगी, तब तक कोई व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता, उसके अन्त:स्थल में घोर अशान्ति घुसी रहेगी। आमतौर से लोग इसी अशान्ति में ग्रसित रहते हैं और पर्याप्त साधन सम्पन्न होते हुए भी मनुष्य जन्म जैसे अमूल्य सौभाग्य से कुछ लाभ नहीं उठा पाते। आन्तरिक विरोधों से उत्पन्न हुई गुत्थियाँ भी उनके लिए एक समस्या बन जाती हैं और मृत्यु समय तक सुलझ नहीं पातीं।
गायत्री की पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य आन्तरिक विरोधों को मिटाकर उनमें समस्वरता की स्थापना करना है। अन्तर में सत्-असत् की रस्साकशी होती है, देवासुर संग्राम, राम-रावण युद्ध, महाभारत होता रहता है। यह कलह तभी शान्त हो सकता है, जब एक पक्ष अशक्त हो जाय। असुर का, असत् का पक्ष ग्रहण करके यदि सत् को पूर्णतया कुचलने का प्रयत्न किया जाए तो वह सम्भव भी नहीं, क्योंकि असुरता स्वयं एक विपत्ति होने के कारण अपने आप अनेक संकट उत्पन्न कर लेती है। दूसरे सत् की स्थिति आत्मा में इतनी सुदृढ़ है कि उसे पूर्णतया कुचलना सम्भव नहीं है। इसलिए आन्तरिक संघर्षों की समाप्ति का एक ही उपाय है—सत् का समर्थन एवं पोषण करके उसे इतना प्रबल कर लिया जाय कि असत् को उससे संघर्ष का साहस ही न हो। लड़ाकू बकरा जब अपने सामने सिंह को खड़ा देखेगा, तो उसे लड़ने की हिम्मत न होगी। आसुरी तत्त्व तभी तक प्रबल रहते हैं, जब तक दैवी तत्त्व कमजोर होते हैं। जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लिया जाता है, तो फिर असुरता अपने हथियार डाल देती है और शान्ति का शासन स्थापित हो जाता है।
पञ्चकोशों की जो साधनाएँ पीछे बताई गई हैं, वे मनुष्य की पाँच महाशक्तियों को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोकती हैं, उन्हें नियन्त्रण में लाकर उपयोगी दिशा में लगाती हैं। सर्कस वाले खूँखार शेर-चीतों को जंगल में से पकड़ लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते हैं कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाना तो दूर, उलटे उन साधने वालों को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं। पाँच कोश पाँच शेर हैं। इन्हें साधने के लिए सरकस वालों की तरह गायत्री साधकों को भी अटूट साहस, अविचल धैर्य एवं सतत प्रयत्नशीलता को अपनाना होता है। इस साधना का आरम्भ काफी कठिनाइयों और निराशाओं से भरा हुआ होता है, परन्तु धीरे-धीरे सफलता मिलने लगती है और गायत्री साधक जब इन पाँच महा सिंहों को, पञ्चकोशों को वश में कर लेता है, तो उसे अनन्त ऐश्वर्य एवं अक्षय कीर्ति का लाभ होता है। सरकस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक सिंहों की महत्ता अनेक गुनी है, इसलिए इनके सध जाने पर सरकस वालों की अपेक्षा लाभ भी असंख्य गुने हैं। कायर इस साधना की कल्पना मात्र से डर जाते हैं, पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ परम पुरुषार्थ ही आनन्ददायक होता है।
कोशों के असन्तुलित, अविकसित, अनियन्त्रित रहने से मानव अन्त:करण की विषम स्थिति रहती है। उसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएँ, भावनाएँ और रुचियाँ उभरती एवं दबती रहती हैं। गायत्री साधना से इनमें एकता उत्पन्न होती है और अन्तर के समस्त संकल्प-विकल्पों की उधेड़बुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित गतिशीलता का आविर्भाव होता है। यह व्यवस्थित गतिशीलता जिस दिशा में भी चलेगी, उसी दिशा में आशाजनक सफलता मिलेगी।
योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्पवृक्ष है जिसके कारण वे सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, आवश्यक, लाभदायक एवं आनन्दवर्द्धक हैं। पाँच व्यक्तियों को एक ही व्यक्तित्व से सुसंयुक्त कर देना एक ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा अपनी शक्ति पाँच गुनी हो जाती है। चूँकि यह केन्द्रीकरण सतोगुण के आधार पर किया जाता है, इसलिए सात्त्विक आत्मबल की प्रचण्ड अभिवृद्धि से पञ्चमुखी गायत्री साधना का साधक महामानव, महापुरुष, महाआत्मा बन जाता है।
कीट-पतंगों की तरह सभी जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की तुच्छ क्रियाओं में संलग्न रहकर साँसें पूरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस रीति से तो पशु-पक्षी भी जी लेते हैं। बल्कि इस दृष्टि से अन्य जीव, मनुष्य से कहीं अच्छे जीते हैं। उन्हें ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, छल, दम्भ, काम, क्रोध, कुढ़न, असन्तोष, शोक, वियोग, चिन्ता आदि की आन्तरिक ग्रन्थियों में हर घड़ी झुलसते रहना नहीं पड़ता। वे अनेक प्रकार के पापों की गठरी अपने ऊपर जमा नहीं करते। मनुष्य इन सब बातों में अन्य जीव-जन्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में रहता है। मरते-मरते अन्य जीव-जन्तु अपने मृत शरीर से दूसरों का कुछ भला कर जाते हैं, पर मनुष्य वह भी नहीं कर पाता।
मानव जीवन की जो प्रशंसा और महत्ता है, उसकी आत्मिक विशेषताओं के कारण है। यदि ये विशेषताएँ अपने स्वस्थ रूप में विकसित हों, तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। योग-साधना का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अद्भुत शक्तियाँ छिपी हैं, उनको योग द्वारा इतनी उन्नत दशा तक पहुँचाया जाता है कि मनुष्य में देवत्व की झाँकी होने लगे।
भारतीय जीवन की आदिकाल से यह विशेषता रही है कि उसमें उद्देश्यमय, आदर्शयुक्त, परिमार्जित जीवन को ही प्रधानता दी गई है। इस देश में उस शक्ति को मनुष्य माना जाता रहा है, जो उद्देश्यमय आदर्श जीवन जीता रहा है। अज्ञान, आसक्ति और अभाव से संघर्ष करने का व्रत लेने वाले ही द्विज कहे जाते हैं। जो द्विज नहीं है, अर्थात् जिसने पारमार्थिक जीवन का व्रत नहीं लिया है, उस स्वार्थी, लोभी, विषयी मनुष्य को शूद्र बताकर निन्दा की है और एक प्रकार से उसका अर्द्ध सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आज तो व्यापक रूप से शूद्रता फैली हुई है। गुण, कर्म, स्वभाव से आज चाण्डाल तत्त्व और शूद्रता का विस्तृत प्रसार हो रहा है।
भारतीय संस्कृति की यह अद्भुत महानता है कि वह अपने हर अनुयायी को यह प्रेरणा देती है कि पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों जैसा शिश्नोदरपरायण तुच्छ जीवन न जीये वरन् अपना प्रत्येक क्षण महान् आदर्शों की पूर्ति में लगाए। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, शरीर-निर्वाह की जरूरतों को कम से कम रखे जिससे उनको कमाने में कम से कम समय और श्रम लगे, बचे हुए अवकाश, बुद्धिबल एवं उत्साह को महानता के सम्पादन में लगाया जा सके।
इस सांस्कृतिक प्रेरणा को ऋतम्भरा, प्रज्ञा एवं सद्बुद्धि नाम से पुकारा गया है। इसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री मन्त्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। यह सद्बुद्धि प्राचीनकाल में अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी। इसी से इस भूमि को पुण्यभूमि, तपोभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे। जीवन्मुक्त आत्माएँ ललचा-ललचाकर इस देश में अवतार लेने के लिए मुक्त-धाम से वापस लौट आती थीं। ऋतम्भरा बुद्धि ने इस देश को महान् मानवों से पाट रखा था। विद्या में, बुद्धिबल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में यह देश भरा-पूरा था। कारण कि सद्बुद्धि ने भारतवासियों की अन्त:भूमिका ऐसी परिमार्जित कर दी थी कि उससे भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों का अक्षय भण्डार उद्भव होना स्वाभाविक ही था।
सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति एवं सुख-शान्ति में रोड़ा बनती हैं। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो सुसम्पन्न बनाने के लिए आवश्यक हैं। सद्बुद्धि का एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामन्त्र के एक-एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। वह इतना उज्ज्वल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान का अन्धकार नष्ट हो जाता है। इन २४ अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान-भण्डार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अवगाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बनता है।
गायत्री के अक्षरों में ज्ञान-भण्डार तो भरा हुआ है, इसके अतिरिक्त इस महामन्त्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केन्द्रों में छिपी हुई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ जाग्रत् होती हैं, जिनके कारण दैवी वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद्बुद्धि वाले के लिए यही बड़ा कठिन है कि वह अपने आप अपने कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाए। इस कठिनाई का हल गायत्री महामन्त्र की उपासना द्वारा होता है। जो इस साधना को करते हैं, वे अनुभव करते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन:क्षेत्र में नवीन ज्ञान, नवीन प्रकाश, नवीन उत्साह आश्चर्यजनक रीति से बढ़ा रही है।
यह छोटा सा मन्त्र ‘अमर फल’ के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत का फल खाने से भी मधुर होता है और उसमें अमरता का लाभ भी होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान-विज्ञान बीज रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग से अन्त:करण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगन्ध की लोकोक्ति गायत्री के सम्बन्ध में भली प्रकार चरितार्थ होती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अत्यन्त स्वादिष्ट पौष्टिक दूध प्रचुर परिमाण में निरन्तर देती रहती है। इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक सम्पत्तियों की प्राप्ति भी होती है। इस दुहरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की अधिक महत्ता है। गायत्री की दोनों महत्ताएँ भी कामधेनु की भाँति ही हैं। इसी से उसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं।
भारतवर्ष में शिल्प, कृषि, व्यापार, विज्ञान, रसायन, शस्त्र विद्या आदि भौतिक उन्नतियों के सम्बन्ध में सदैव महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं, आज भी उनकी आवश्यकता है। पूँजी, कुशलता, श्रम एवं सहयोग के आधार पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए और यथासम्भव उन्हें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए भौतिक साधन-सामग्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है। भूखा आदमी न ईमानदार रह सकता है और न स्वस्थ चित्त। इसलिए जीवनयात्रा की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए भौतिक सम्पत्तियों का उपार्जन आवश्यक है, पर यह ध्यान रखने की बात है कि यदि भौतिक उन्नति पर ही एकमात्र ध्यान रखा गया और सम्पत्ति के ऊपर से आत्मिक नियन्त्रण उठा दिया गया, तो जो कुछ सांसारिक उन्नति होगी, वह केवल मनुष्य की आपत्तियाँ बढ़ाने का कारण बनेगी।
इन दिनों विज्ञान का बड़ा जोर है, सुविधाओं के साधन नित नए निकलते जा रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य विलासी, आलसी, दुर्बल, रोगी, कायर और अल्पजीवी होता चला जा रहा है। जिन देशों ने अपनी शक्ति बढ़ाई है, वे छोटे देशों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों का परिणाम यह है कि एटम बम, हाइड्रोजन बम संसार में प्रलय उपस्थित करने के लिए तैयार हैं। साधारण लोगों पर दृष्टि डालिए तो उनका भी यही हाल है। भौतिक शक्ति पाकर लोग अपना और दूसरों का विनाश ही करते हैं। वकीलों की विद्या से किसका क्या हित है? ज्यादा कमाने वाले मजदूर शराब और ताड़ी में अपनी कमाई फूँक देते हैं। साहसी स्वभाव और बलवान् शरीर वाले गुण्डा, डाकू, अत्याचारी बनने में अपना गौरव देखते हैं। देहातों में आजकल अन्न की महँगाई से किसानों की आर्थिक दशा थोड़ी सुधरी है, तो फौजदारी, मुकदमेबाजी, विवाह-शादियों आदि बातों में फिजूलखर्ची की बेतरह बाढ़ आ गई है। यह निश्चित है कि यदि भौतिक उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश न होगा, तो वह भस्मासुर के वरदान की तरह अपना ही सर्वनाश करने वाली सिद्ध होगी। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ-साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए। सुन्दर बहुमूल्य वस्त्राभूषण तभी शोभा पाते हैं, जब पहनने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो। मरणासन्न अस्थिपंजर रोगी को यदि रेशमी कपड़ों से और जेवर से लाद दिया जाए, तो उसकी शोभा तो कुछ न बढ़ेगी, उलटे उसकी असुविधा बढ़ जाएगी। आत्मिक उन्नति के बिना भौतिक सम्पदाओं की बढ़ोत्तरी से मनुष्य की अहंकारिता, ईर्ष्या, विलासिता, कुरुचि, चिन्ता, कुढ़न, शत्रुता आदि कष्टकारक बुराइयाँ भी बढ़ जाती हैं।
गायत्री आत्मोन्नति का, आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सांसारिक सम्पत्तियाँ उपार्जन करना जिस प्रकार आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार गायत्री-साधना द्वारा आत्मिक पूँजी बढ़ाने का प्रयत्न भी निरन्तर जारी रहना चाहिए। दोनों दिशाओं में साथ-साथ सन्तुलित विकास होगा तो स्वस्थ उन्नति होगी, किन्तु यदि केवल धन या भोग के सञ्चय में ही लगा रहा गया, तो निश्चित है कि वह कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकट्ठी भले ही दीखे, पर उसमें वास्तविक सुख की उपलब्धि तनिक भी न हो सकेगी। जो सांसारिक वस्तुओं का समुचित लाभ उठाना चाहता हो, उसे चाहिए कि आत्मोन्नति के लिए उतना ही प्रयत्न करे।
आँखों के बिना सुन्दर दृश्य देखने का लाभ नहीं मिल सकता, कान बहरे हों तो मधुर संगीत का रसास्वादन सम्भव नहीं। आत्मिक शक्ति न हो ,तो सांसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लाभ नहीं उठाया जा सकता है। सुन्दर दृश्य और तीव्र नेत्र ज्योति के संयोग से ही चित्त प्रसन्न होता है। भौतिक और आत्मिक उन्नति का समन्वय ही जीवन में सुस्थिर शान्ति की स्थापना कर सकता है। हम धन कमाएँ, विद्या पढ़ें और उन्नति करें, पर यह न भूलें कि इसका वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा, जब आत्मोन्नति के लिए भी समुचित साधना की जा रही हो।
१-स्वास्थ्य, २-धन, ३-विद्या, ४-चतुरता, ५-सहयोग, यह पाँच सम्पत्तियाँ इस संसार में होती हैं। इन्हीं पाँच के अन्तर्गत समस्त प्रकार के वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार पाँच कोशों की परिमार्जित स्थिति ही पाँच आध्यात्मिक सम्पदाएँ हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय—यह पाँच कोश आध्यात्मिक शक्तियों के पाँच भण्डार हैं। इन कोशों पर जो अधिकार कर लेता है, उसकी अन्त:चेतना का पञ्चीकरण हो जाता है और १-आत्मज्ञान, २-आत्मदर्शन, ३-आत्मानुभव, ४-आत्मलाभ, ५-आत्मकल्याण, यह पाँच आध्यात्मिक सम्पदाएँ प्राप्त हो जाती हैं।
गायत्री के चित्र में दस भुजाएँ दिखाई गई हैं—पाँच बायीं और पाँच दाहिनी ओर। बायीं ओर की पाँच भुजाएँ सांसारिक सम्पत्तियाँ हैं और दाहिनी ओर की भुजाएँ पाँच आत्मिक शक्तियाँ हैं। गायत्री उपासक इन दसों लाभों को प्राप्त करके रहता है।
(१) ‘आत्मज्ञान’ का अर्थ है—अपने को जान लेना, शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेना और शारीरिक लाभों को आत्मलाभ की तुलना में उतना ही महत्त्व देना जितना कि दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर हो जाता है। इन्द्रिय भोगों की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अनुचित, अनावश्यक व्यय होता है, जिससे शरीर असमय में ही दुर्बल, रोगी, कुरूप एवं जीर्ण हो जाता है। आत्मज्ञानी इन्द्रिय भोगों की उपयोगिता-अनुपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ की दृष्टि से करता है, इसलिए वह स्वभावत: संयमी रहता है और शरीर से सम्बन्ध रखने वाले दु:खों से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं कुरूपता का कष्ट उसे नहीं भोगना पड़ता। जो कष्ट उसे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं, वह भी आसानी से भुगत जाते हैं।
(२) ‘आत्मदर्शन’ का तात्पर्य है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है, तब प्रीति-प्रतीति, श्रद्धा-निष्ठा और विश्वास की भावनाएँ बढ़ती हैं। कभी भौतिकवादी, कभी अध्यात्मवादी होने की डावाँडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण, कर्म, स्वभाव प्रकट होने लगते हैं, जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित हैं। उस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका में पहुँचने पर दूसरों को जानने, समझने और उन्हें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है।
जिसे आत्मदर्शन हुआ है उसकी आत्मिक सूक्ष्मता अधिक व्यापक हो जाती है, वह संसार के सब शरीरों में अपने को समाया हुआ देखता है। जैसे अपने मनोभाव, आचरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरों के भीतर की सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती हैं। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन से काम लेने में समर्थ होते हैं, वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीरों पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है।
(३) ‘आत्मानुभव’ कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना, अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार पर ही अपनी वाणी, क्रिया, योजना, इच्छा, आकांक्षा, रुचि एवं भावना का होना। आमतौर से लोग विचार तो बहुत ऊँचे रखते हैं, पर बाह्य जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते। उनका व्यावहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है। किन्तु जिन्हें आत्मानुभव होता है, वे भीतर-बाहर एक होते हैं। उनके विचार और कार्यों में तनिक भी अन्तर नहीं होता। जो विघ्न-बाधाएँ सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ती हैं, उन्हें वे एक ठोकर से तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है।
आत्म-अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिलती है। किसका क्या भविष्य बन रहा है? भूतकाल में कौन क्या कर रहा है? किस कार्य में दैवी प्रेरणा क्या है? क्या उपद्रव और भय उत्पन्न होने वाले हैं? लोक-लोकान्तरों में क्या हो रहा है? कब, कहाँ, क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है? आदि ऐसी अदृश्य एवं अज्ञात बातें, जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते, उन्हें आत्मानुभव की भूमिका में पहुँचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है। आरम्भ में उसे अनुभव कुछ धुँधले होते हैं, पर जैसे-जैसे उनकी दिव्यदृष्टि निर्मल होती जाती है, सब कुछ चित्रवत् दिखाई देने लगता है।
(४) ‘आत्मलाभ’ का अभिप्राय है-अपने में पूर्ण आत्मतत्त्व की प्रतिष्ठा। जैसे भट्ठी में पड़ा लोहा तपकर अग्निवर्ण सा लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुँचा हुआ सिद्ध पुरुष दैवी तेजपुञ्ज से परिपूर्ण हो जाता है। वह सत् की प्रत्यक्ष मूर्ति होता है। जैसे अँगीठी के पास बैैठने से गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही महापुरुषों के आस-पास ऐसा सतोगुणी वातावरण छाया रहता है, जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शान्ति अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में ग्रीष्म की धूप से तपे हुए लोगों को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेक दु:खियों को शान्ति प्रदान करते रहते हैं।
आत्मलाभ के साथ-साथ आत्मा की-परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों से सम्बन्ध हो जाता है। परमात्मा की एक-एक शक्ति का प्रतीक एक-एक देवता है। यह देवता अनेक ऋद्धि-सिद्धियों का अधिपति है। ये देवता जैसे विश्व-ब्रह्माण्ड में व्यापक हैं, वैसे ही मानव शरीर में भी हैं। विश्व-ब्रह्माण्ड का ही एक छोटा सा रूप यह पिण्ड देह है। इस पिण्ड देह में जो दैवी शक्तियों के गुह्य संस्थान हैं, वे आत्मलाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वह उन दैवी शक्तियों से इच्छानुसार कार्य ले सकता है।
(५) ‘आत्मकल्याण’ का अर्थ है—जीवन-मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अक्षय आनन्द, ब्रह्मनिर्वाण, स्थित-प्रज्ञावस्था, परमहंस -गति, ईश्वर -प्राप्ति। इस पञ्चम भूमिका में पहुँचा हुआ साधक ब्राह्मीभूत होता है। इसी पञ्चम भूमिका में पहुँची हुई आत्माएँ ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती हैं। उन्हें देवदूत, अवतार, पैगम्बर, युगनिर्माता, प्रकाश स्तम्भ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज ऐसी नहीं, जो उन्हें अप्राप्य हो। वे अक्षय आनन्द के स्वामी होते हैं। ब्रह्मानन्द, परमानन्द एवं आत्मानन्द से बड़ा और कोई सुख इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में सम्भव नहीं; यही सर्वोच्च लाभ आत्मकल्याण की भूमिका में पहुँचे हुए को प्राप्त हो जाता है।
दशभुजी गायत्री की पाँच भुजा सांसारिक हैं, पाँच आत्मिक। आत्मिक भुजाएँ, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मानुभव, आत्मलाभ और आत्मकल्याण हैं। यह दैवी सम्पदाएँ जिनके पास हैं, उनके वैभव की तुलना कुबेर से भी नहीं हो सकती। गायत्री का उपासक आत्मिक दृष्टि से इतना सुसम्पन्न और परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी तुलना किन्हीं भी सांसारिक सम्पदाओं से नहीं की जा सकती। ये पाँचों भूमिकाएँ, सिद्धियाँ, पञ्चकोशों से सम्बन्धित हैं। एक-एक कोश की साधना एक-एक भूमिका में प्रवेश कराती जाती है। अन्नमय कोश का साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। प्राणमय कोश की साधना से आत्मदर्शन होता है, मनोमय कोश के साथ आत्मानुभव होता है, विज्ञानमय कोश से आत्मलाभ का सम्बन्ध है और आनन्दमय कोश में आत्मकल्याण सन्निहित है।
दशभुजी गायत्री की पाँच भुजाएँ सूक्ष्म और पाँच स्थूल हैं। निष्काम उपासना करने वाले माता के सूक्ष्म हाथों से आशीर्वाद पाते हैं और सकाम उपासकों को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने माता की कृपा से सांसारिक सम्पत्तियाँ प्राप्त की हैं और अपनी दुर्गम कठिनाइयों से त्राण पाया है। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग, ये पाँच सांसारिक सम्पत्तियाँ पञ्चमुखी माता की स्थूल भुजाओं से मिलती हैं।
ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं, जिनमें लोगों ने साधारण गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलताएँ प्राप्त की हैं। जिनके घर में रोग घुस रहा था, बीमारी की पीड़ा सहते-सहते और डॉक्टरों का घर भरते-भरते जो कातर हो रहे थे, उन्होंने रोगमुक्ति के वरदान पाए। क्षय सरीखे प्राणघातक रोगों की मृत्युशय्या पर से उठकर खड़े हो गए। कइयों को जन्मजात पैतृक रोगों तक से छुटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति अच्छी जीविका के अधिकारी बन गए। साधनहीन और अविकसित लोग चतुर, बुद्धिमान्, कलाकार, शिल्पी, गुणवान्, प्रतिभावान्, सर्वप्रिय नेता और यशस्वी बन गए। जिनको सब ओर से तिरस्कार, अपमान, द्वेष, संघर्ष और असहयोग ही मिलता था, उनको घर-बाहर सर्वत्र प्रेम, सहयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा।
ऐसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं परिचित हैं। मुकदमा, आक्रमण, बन्धन, भय, आशंका, विरोध, परीक्षा, बीमारी, दरिद्रता, भूत-बाधा, सन्तति-कष्ट, व्यसन, दुर्गुण आदि कुचक्रों के त्रासदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यक्तियों ने सन्तोष की साँस ली है। कष्टकर वर्तमान और भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो रहे थे, उन्होंने जब गायत्री का आश्रय लिया तो तत्क्षण उन्हें धैर्य, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ। यह ठीक है कि कोई देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया, पर यह भी सत्य है कि उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई, जिससे झट बिगड़ा काम बन गया और पर्वत-सी भारी कठिनाई राई की तरह छोटी होकर हल हो गई। जिस आपत्ति में यह लगता था कि न जाने इसके कारण हम पर क्या बीतेगी, वह सब आशंकाएँ काई की तरह फट गईं और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं।
स्वास्थ्य और धन की ही भाँति दशभुजी गायत्री की तीसरी स्थूल भुजा का प्रसाद ‘विद्या’ के रूप में मिलता है। मन्दबुद्धि, मूढ़मगज, भुलक्कड़, मूर्ख, अदूरदर्शी, सिड़ी, सनकी एवं अर्द्धविक्षिप्त मनुष्यों को बुद्धिमान्, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान् बनते देखा गया है। जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई यह भविष्यवाणी करता था कि अपना पेट भी न भर सकेंगे, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गए, लोग उनकी सलाह लेकर काम करने में अपनी भलाई समझने लगे।
जिनकी पढ़ाई में रुचि न थी, वे पुस्तकों के कीड़े हो गए। हर साल फेल होने वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से ऐसे तीव्र बुद्धि के हुए कि सदैव अच्छे नम्बरों से उन्हें सफलता मिलती गई। अनेक उलझनें, कार्यव्यस्तता एवं अवकाश का अभाव रहने पर भी कितने ही साधनहीन व्यक्ति विद्वान् बने हैं। मस्तिष्क से काम लेने वाले कितने ही बुद्धिजीवी मनुष्य ऐसे हैं, जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यन्त प्रखर बनाया है और फलस्वरूप वे उज्ज्वल नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए हैं। अपने बुद्धिबल से उन्होंने आशाजनक सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति और सम्पदा उपार्जित की है।
विकृत मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजा के प्रसाद से स्वस्थ मनोभूमि प्राप्त करते हैं। भूतोन्माद, प्रेतबाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत शक्ति गायत्री उपासना में है। हजार ओझा, सयाने और तान्त्रिक तराजू के एक पलड़े में रखे जाएँ और एक गायत्री उपासक एक ओर रखा जाए, तो निश्चित रूप से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध होगी।
चातुर्यपूर्ण कामों का आरम्भ करते समय शारदा का, सरस्वती का आह्वान, वन्दन और पूजन करने की प्रथा है। कारण यही है कि बुद्धि तत्त्व में माता की कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है, जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयंगम हो जाती हैं। चित्रकला, संगीत, कविता, सम्भाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, शिक्षण, नेतृत्व, अन्वेषण, परीक्षण, निर्णय, दलाली, प्रचार, व्यवसाय, खेल, प्रतिद्वन्द्विता कूटनीति आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं, जिनमें विशेष सफलता वही पा सकता है जिसकी बुद्धि में सूक्ष्मता हो। मोटी अक्ल से इस प्रकार के कर्मों में लाभ नहीं होता। कुशाग्र, सूक्ष्मवेधी बुद्धि-चातुर्य गायत्री माता के पुण्य-प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्यों को आरंभ करते हुए शारदा-वन्दना करते हैं।
गायत्री की स्थूल पाँच भुजाओं में पाँचवीं भुजा का प्रसाद सहयोग है। यह जिसे मिलता है, वह स्वयं विनम्र, मधुरभाषी, प्रसन्नचित्त, हँसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहृदय, सेवाभावी, निरहंकारी बन जाता है। ये विशेषताएँ उनमें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, फलस्वरूप उनके संपर्क में जो भी कोई आता है, वह उनका बेपैसे का गुलाम बन जाता है। ऐसे स्वभाव के मनुष्य के स्त्री, पुरुष, पुत्र, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ सभी अनुकूल, सहायक और प्रशंसक रहते हैं। घर में उसका मान-सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। घर में हों, बाहर बाजार में, मित्रों में, परिचितों में, सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति कहीं भी मित्रविहीन नहीं रहते। वे जहाँ भी रहते हैं, वहीं उन्हें प्रेमी, प्रशंसक, मित्र, सहायक-सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं।
दाहिनी और बाईं, सूक्ष्म और स्थूल गायत्री की दस भुजाएँ साधक को प्राप्त होने वाली पाँच आत्मिक और पाँच भौतिक सिद्धियाँ हैं। ये दस सिद्धियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा यही जीवन, यही लोक स्वर्गीय सुख से ओत-प्रोत हो जाता है। यह जीवन अगले जीवन की पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज संतुष्ट है तो कल भी उसे संतोष ही उपलब्ध होगा, यदि आज उसे कल्याण का अनुभव होता है तो कल कल भी कल्याण ही होगा। सत्पुरुष अक्सर दुस्साहसपूर्ण और वर्तमान वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं, इसलिए बाह्य दृष्टि से उन्हें कुछ असुविधाएँ दिखाएँ देती हैं। परन्तु उनकी आन्तरिक स्थिति पूर्ण प्रसन्न और सन्तुष्ट होती है। ऐसी दशा में यह भी निश्चित है कि उनका अगला जीवन भी पूर्णतया प्रसन्नता एवं संतोष की भूमिका में और भी अधिक विकसित होगा और आज की बाह्य कठिनाइयाँ भी कल तक स्थिर न रहेंगी।
क्या योग साधना के लिए घर-गृहस्थ छोड़कर साधु बनना, कपड़े रँगना, यत्र-तत्र भ्रमण करते रहना आवश्यक है? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पूर्वकाल के योगियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्राचीनकाल में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे, यह मान्यता ठीक नहीं। यह ठीक है कि ऋषि-मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे, यह बात भी बिलकुल ठीक है। स्त्री-बच्चों के साथ होने से उन्हें तपश्चर्या एवं आत्मोन्नति में सहायता मिलती थी।
इतिहास-पुराणों में पग-पग पर इस बात की साक्षी मिलती है कि भारतीय महर्षिगण योगी, यती, साधु, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रचयिता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेता आदि विविध रूपों में अपना जीवन यापन करते थे और इन महान् कार्यों में स्त्री-बच्चों को भी अपना भागीदार बनाते थे।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विवाहित थे। ब्रह्मा की गायत्री और सावित्री दो स्त्रियाँ थीं। विष्णु की तुलसी और लक्ष्मी दो पत्नी हैं। सती के मरने के बाद महादेव जी का दूसरा विवाह पार्वती से हुआ था। व्यास, अत्रि, गौतम, वसिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, च्यवन आदि सभी ऋषि गृहस्थ ही थे। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ गार्गी और मैत्रेयी थीं। अत्रि की पत्नी अनसूया अपने समय की प्रमुख ब्रह्मवादिनी थी। ऐसे प्रमाणों से इतिहास-पुराणों का पन्ना-पन्ना भरा पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में योगी लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते थे।
उस समय की परिस्थितियाँ, प्रथाएँ, सुविधाएँ तथा सादगी की पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्त्विक जीवन बिताते थे। वेश बनाने या घर छोड़ने की उनकी कोई योजना न थी। लकड़ी की खड़ाऊँ, तुम्बी का जलपात्र उनकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे। उस समय आबादी कम और वन अधिक थे। आसानी से बन सकने वाली झोंपड़ी, छोटे-छोटे ग्राम उस समय की साधारण परिपाटी थी। पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में उन बातों की नकल करना कहाँ तक उचित है, यह पाठक स्वयं सोच सकते हैं।
उस समय दूध पीकर फल खाकर रहने वाले लोग त्यागी नहीं समझे जाते थे, क्योंकि विस्तृत वनों में चरने की सुविधा होने से कोई मनुष्य कितनी ही गाएँ पाल सकता था। जंगलों मे अपने आप उगे फलों को लाने में कोई बाधा न थी। पर आज तो एक गाय पालने में एक परिवार के बराबर खर्च आता है। पेट को खराब कर डालने वाले फलों को न लेकर यदि सुखाद्य फलों को लिया जाए, तो भी काफी खर्च होता है। जो बात उस समय अत्यन्त सादगी की थी, वह आज अमीरों के लिए भी दुर्लभ है।
रास्ते रोके पड़ी रहने वाली, टूटे हुए वृक्षों की सूखी लकड़ी को साफ करने तथा हिंसक जानवरों का आक्रमण रोकने के लिए दिन-रात ‘धूनी’ जलाई जाती थी। पर आज तो लकड़ी का भाव इतना अधिक है जिसे किसी भी स्थिति में वहन नहीं किया जा सकता। उस समय स्वाभाविक मृत्यु से मरते रहने वाले मृग आदि जीवों का चमड़ा चाहे जितना मिलता था। पर आज तो बिना हत्या का चमड़ा प्राप्त करना असंभव-सा लगता है। फिर एक मृगचर्म का मूल्य भी कल्पनातीत है। इतने रुपए से तो कुश के ढेरों आसन खरीदे जा सकते हैं। सर्दी-गर्मी से बचने के लिए देह पर भस्म मलने से, भभूत रमाने से काम चल जाता था। वस्त्र वहाँ जंगलों में थे नहीं। पर आज जब वस्त्रों का मिलना सुगम है, तो भभूत लगाने की क्या आवश्यकता है?
उस जमाने में पेड़ काटने, अग्नि सँभालने, जंगली पशुओं से मुकाबला करने के लिए बड़ा-सा चिमटा रखना आवश्यक था, पर आज जब कि वह तीनों ही कारण नहीं रहे, तो चिमटे का क्या प्रयोजन रह गया? पूर्वकाल में जिन बातों को सादगी एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक आवश्यक समझा जाता था, आज की परिस्थितियों में उनमें से कितनी ही बातें अनावश्यक हैं। हमने भारतवर्ष की एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार आध्यात्मिक यात्राएँ की हैं। अपने अनुभव के बल पर हम कह सकते हैं कि अब कोई वन ऐसा नहीं रहा है, जहाँ फल खाकर या अपने आप चरकर आने वाली गौओं का दूध पीकर कोई व्यक्ति गुजारा कर सके, न आज के मनुष्यों के शरीर ही ऐसे हैं कि शीत प्रधान देशों में मकान या वस्त्रों के बिना रह सकें। जो योगी-यती गंगोत्री आदि में रहते हैं, उनको भी वस्त्र, मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है।
भिक्षाजीवी होकर, दूसरों से ऋण लेकर आज की अभावग्रस्त जनता पर, अश्रद्धालु जनता पर भार बनकर ‘साधु’ वेश बना लेना, बदली हुई परिस्थितियों का विचार न करके पूर्वजों की वेशभूषा का अन्धानुकरण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। साधु हो जाने वालों को भी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है, जितना कि गृहस्थ को। ऐसी दशा में यही उचित है कि अपनी जीविका की आप व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सादा वेश में साधु जीवन व्यतीत किया जाए।
साधना मन से होती है न कि वेश से। मन तो भारी भीड़ में भी शांत रह सकता है और एकांत वन में भी विकारग्रस्त हो सकता है, फिर एकांतसेवी लोगों की इंद्रिय-विजय भी कच्ची होती है। जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलता, वह ईमानदार है। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रलोभन के वक्त वह फिसल सकता है। जिसको चोरी के सदा अवसर हैं, फिर भी अपने पर काबू रखता है, उसी को विश्वस्त, प्रमाणिक, ईमानदार कहा जाएगा। एकान्त जंगल में बैठकर, लोगों से संबंध तोड़कर कोई व्यक्ति बुराइयों से बच जाए, तो उसके संस्कार उतने सुदृढ़ नहीं हो सकते जितने कि निरन्तर बुराइयों से संघर्ष करके अपनी अच्छाई को विकसित करने वाले के होते हैं। शूर की परीक्षा युद्धभूमि में होती है। घर में बैठा हुआ तो मरीज भी तीसमारखाँ कहला सकता है।
गायत्री-साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उन्नति करने एवं कल्याण-पथ पर चलने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं कि कोई विचित्र वेश बनाया जाए, घर-द्वार छोड़कर भीख के टूँकों पर गुजारा किया जाए। कुछ विशिष्ट आत्माएँ संन्यास की अधिकारी होती हैं। वह अधिकार तब मिलता है, जब साधना पूर्ण परिपक्व होकर मनोभूमि इस योग्य हो जाती है कि वह संसार का पथ-प्रदर्शन करने के लिए परिव्राजक बने। साधारण साधकों के लिए यह मार्ग ग्रहण करना अनधिकार चेष्टा करना है।
गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, निश्चित आहार-विहार की सुविधा घर छोड़ने वाले को नहीं हो सकती। पात्र-कुपात्रों का अन्न, पेट में जाकर बुद्धि पर तरह-तरह के संस्कार डालता है, इसलिए अपने परिश्रम की कमाई हुई रोटी पर गुजारा करते हुए गृहस्थ जीवन में ही साधनाक्रम का आयोजन करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य उचित और आवश्यक है, जिससे जितना संयम हो सके उतना अच्छा है। पुरश्चरण की निश्चित अवधि में जब तक निश्चित संकल्प का जप पूरा न हो, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। परन्तु नियतकालीन निर्धारण संख्या या अवधि के विशेष पुरश्चरणों को छोड़कर, सामान्य साधनाक्रम में ब्रह्मचर्य अनिवार्य शर्त नहीं है। गृहस्थ लोग अपने साधारण एवं स्वाभाविक दाम्पत्य कर्त्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपनी साधना जारी रख सकते हैं। इससे उनके साधन में कोई बाधा न आएगी।
मन पर नियन्त्रण करने की सात्त्विकता के नियम पालन करने की सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। जहाँ पानी होगा, वहीं तो तैरना सीखा जाएगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला अच्छा तैराक किस प्रकार बन सकेगा? तैरने की अनेक शिक्षाएँ ग्रहण करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक कि वह पानी में रहकर भी न डूबने की अपनी योग्यता प्रमाणित न कर दे। गृहस्थ जीवन में अनेक अनुकूल-प्रतिकूल, भले-बुरे, हर्ष-विषाद के अवसर आते हैं, उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन के साधन से स्वभाव और संस्कारों में प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आती है।
अपने बुरे संस्कारों एवं स्वभावों से नित्य संघर्ष करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए घोर प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर प्रयत्न एवं संघर्ष को मन्थन कहते हैं। इसे ही गीता में ‘धर्मयुद्ध’ या ‘कर्मयोग’ कहा है। अर्जुन चाहता है-हमारा अज्ञानग्रस्त मन कहता है कि इस झंझट से दूर रहकर, एकान्तवासी बनकर सफलता का कोई दूसरा मार्ग मिल जाए। वह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि संघर्ष सदा ही कष्टसाध्य होता है। मनुष्य की कायर प्रकृति सदा उससे बचना चाहती है। कायर सिपाही सदा ही लड़ाई के मोर्चे से भाग खड़े होने की योजना बनाते हैं। इसी प्रकार अपने स्वभाव की, परिवार की, समाज की, देश-काल की परिस्थितियों से खीजकर कई आदमी निराश होकर बुराइयों को आत्मसमर्पण ही कर देते हैं।
इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान् ने बुरी तरह लताड़ा था और उसके तर्कों में झाँकती हुई कायरता का पर्दाफाश कर दिया था। भगवान् ने कहा—‘‘बिना लड़े कल्याण नहीं, सफलता-असफलता की बात को मन से हटाकर लड़ने को अपने कर्त्तव्य मानकर तू लड़।’’ साधकों के लिए भी यही मार्ग है। विपरीत परिस्थितियों से उन्हें निरन्तर अति उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इतना प्रयत्न करने पर भी कम सफलता मिली, यह सोचना धर्मयुद्ध के विज्ञान के विपरीत है। संघर्ष एक साधना है। उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। मन्थन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। साधन-समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों न हो, प्रगति चाहे कितनी मन्द क्यों न हो, पर यह ध्रुव निश्चय है कि यदि साधक की यात्रा उसी दशा में जारी है, तो वह आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके रहेगा।
Versions
-

ENGLISHSuper Science of GayatriScan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानScan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 1Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 2Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 3Scan Book Version
-
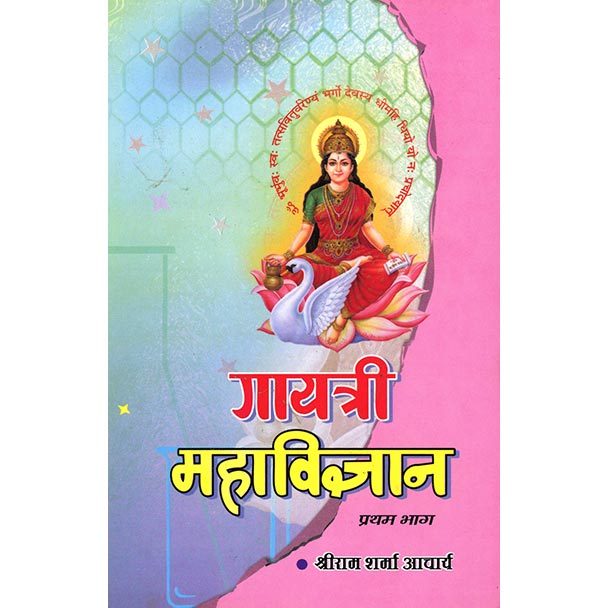
MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग १Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग २Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग ३Scan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानText Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग)Text Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान भाग 2Text Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री महाविज्ञान भाग १
- वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति
- ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव
- गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है
- गायत्री साधना से शक्तिकोशों का उद्भव
- शरीर में गायत्री मंत्र के अक्षर
- गायत्री और ब्रह्म की एकता
- महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान
- त्रिविध दु:खों का निवारण
- गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना
- गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता
- गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण
- जीवन का कायाकल्प
- नारियों को वेद एवं गायत्री का अधिकार
- देवियों की गायत्री साधना
- गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य
- गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत (जनेऊ)
- साधकों के लिये उपवीत आवश्यक है
- गायत्री साधना का उद्देश्य
- निष्काम साधना का तत्त्व ज्ञान
- गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध
- साधना- एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- आत्मशक्ति का अकूत भण्डार :: अनुष्ठान
- सदैव शुभ गायत्री यज्ञ
- महिलाओं के लिये विशेष साधनाएँ
- एक वर्ष की उद्यापन साधना
- गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि
- गायत्री का अर्थ चिन्तन
- साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते
- साधना की सफलता के लक्षण
- सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिये
- गायत्री द्वारा कुण्डलिनी जागरण
- यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बाँटिये
- गायत्री महाविज्ञान भाग ३ भूमिका
- गायत्री के पाँच मुख
- अनन्त आनन्द की साधना
- गायत्री मञ्जरी
- अन्नमय कोश और उसकी साधना
- उपवास - अन्नमय कोश की साधना
- आसन - अन्नमय कोश की साधना
- तत्त्व शुद्धि - अन्नमय कोश की साधना
- तपश्चर्या - अन्नमय कोश की साधना
- मनोमय कोश की साधना
- ध्यान - मनोमय कोश की साधना
- त्राटक - मनोमय कोश की साधना
- जप - मनोमय कोश की साधना
- तन्मात्रा साधना - मनोमय कोश की साधना
- विज्ञानमय कोश की साधना
- सोऽहं साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मानुभूति योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मचिन्तन की साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- स्वर योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- वायु साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- ग्रन्थि-भेद - विज्ञानमय कोश की साधना
- आनन्दमय कोश की साधना
- नाद साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- बिन्दु साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- कला साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- तुरीयावस्था - आनन्दमय कोश की साधना
- पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य
- गायत्री-साधना निष्फल नहीं जाती
- पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य
- गायत्री का तन्त्रोक्त वाम-मार्ग
- गायत्री की गुरु दीक्षा
- आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- मन्त्र दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- अग्नि दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्म दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- कल्याण मन्दिर का प्रवेश द्वार - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्मदीक्षा की दक्षिणा आत्मदान - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- वर्तमानकालीन कठिनाइयाँ - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ

