गायत्री महाविज्ञान 
अग्नि दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
Read Scan Version
दूसरी ‘भुव:’ भूमिका में पहुँचने पर दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है। इसे प्राण-दीक्षा या अग्नि-दीक्षा कहते हैं। प्राणमय कोश एवं मनोमय कोश के अन्तर्गत छिपी हुई शक्तियों को जाग्रत् करने की साधना का शिक्षण क्षेत्र यही है। साधना संग्राम के अस्त्र-शस्त्रों को धारण करना, सँभालना और चलाना इसी भूमिका में सीखा जाता है। प्राणशक्ति की न्यूनता का उपचार इसी क्षेत्र में होता है। साहस, उत्साह, परिश्रम, दृढ़ता, स्फूर्ति, आशा, धैर्य, लगन आदि वीरोचित गुणों की अभिवृद्धि इसी दूसरी भूमिका में होती है। मनुष्य शरीर के अन्तर्गत ऐसे अनेक चक्र, उपचक्र, भ्रमर, उपत्यिका, सूत्र प्रत्यावर्तन, बीज, मेरु आदि गुप्त संस्थान होते हैं, जो प्राणमय भूमिका की साधना से जाग्रत् होते हैं। इस जागरण के फलस्वरूप साधक में ऐसी अनेक विशेषताएँ उत्पन्न हो जाती हैं जैसी कि साधारण मनुष्यों में नहीं देखी जातीं।
भुव: भूमिका में ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के चतुष्टय का संशोधन, परिमार्जन एवं विकास होता है। यह सब कार्य मध्यमा और पश्यन्ती वाणी द्वारा किया जाता है। वैखरी वाणी द्वारा वचनों के माध्यम से प्रारम्भिक साधक को ‘भू:’ क्षेत्र के मन्त्र दीक्षित को सलाह, शिक्षा आदि दी जाती है। जब प्राण दीक्षा होती है, तो गुरु अपना प्राण शिष्य के प्राण में घोल देता है, बीज रुप से अपना आत्मबल साधक के अन्त:करण में स्थापित कर देता है। जैसे आग से आग जलायी जाती है, बिजली की धारा से बल्व जलते या पंखे चलते हैं, उसी प्र्रकार अपना शक्ति-भाग बीज रूप से दूसरे की मनोभूमि में जमाकर वहाँ उसे सींचा और बढ़ाया जाता है। इस क्रिया पद्धति को अग्नि दीक्षा कहते हैं। अशक्त को सशक्त बनाना, निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराश को आशान्वित करना प्राण दीक्षा का काम है। मन से विचार उत्पन्न होता है, अग्नि से क्रिया उत्पन्न होती है। अन्त:भूमि में हलचल, क्रिया, प्रगति, चेष्टा, क्रान्ति, बेचैनी, आकांक्षा का तीव्र गति से उदय होता है।
साधारणत: लोग आत्मोन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं देते, थोड़ा-सा देते हैं तो उसे बड़ा भारी बोझ समझते हैं, कुछ जप तप करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है मानो बहुत बड़ा मोर्चा जीत रहे हों। परन्तु जब आन्तरिक स्थिति भुव: क्षेत्र में पहुँचती है, तो साधक को बड़ी बेचैनी और असन्तुष्टि होती है। उसे अपना साधन बहुत साधारण दिखाई पड़ता है और अपनी उन्नति उसे बहुत मामूली दीखती है। उसे छटपटाहट उवं जल्दी होती है कि मैं किस प्रकार शीघ्र लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। अपनी उन्नति चाहे कितनी ही सुव्यवस्थित ढंग से हो रही हो, पर उसे सन्तोष नहीं होता। यह व्याकुलता उसकी कोई भूल नहीं होती वरन् भीतर ही भीतर जो तीव्र क्रिया शक्ति काम कर रही है उसकी प्रतिक्रिया है। भीतरी क्रिया, प्रवृत्ति और प्रेरणा का बाह्य लक्षण असन्तोष है। यदि असन्तोष न हो, तो समझना चाहिए कि साधक की क्रिया शक्ति शिथिल हो गई। जो साधक दूसरी भूमिका में है, उसका असन्तोष जितना ही तीव्र होगा, उतनी ही क्रिया शक्ति तेजी से काम करती रहेगी। बुद्धिमान् पथ-प्रदर्शक दूसरी कक्षा के साधक में सदा असन्तोष भड़काने का प्रयत्न करते हैं ताकि आन्तरिक क्रिया और भी सतेज हो, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह असन्तोष कहीं निराशा में परिणत न हो जाय।
अग्नि दीक्षा लेकर साधक का आन्तरिक प्रकाश स्वच्छ हो जाता है और उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अँधेरे में, धुँधले प्रकाश में बड़ी वस्तुयें ही ठीक प्रकार दीखती हैं और कई बार तो प्रकाश की तेजी के कारण वे वस्तुएँ और भी अधिक महत्त्वपूर्ण दीखती हैं। आत्मा में ज्ञानाग्नि का प्रकाश होते ही साधक को अपनी छोटी-छोटी भूल, बुराई, कमियाँ भली प्रकार दीख पड़ती हैं। उसे मालूम पड़ता है कि मैं असंख्य बुराइयों का भण्डार हूँ, नीची श्रेणी के मनुष्यों से भी मेरी बुराइयाँ अधिक हैं। अब भी पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते। इस प्रकार वह अपने अन्दर घृणास्पद तत्त्वों को बड़ी मात्रा में देखता है। जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के लोग कतई गलती नहीं मानते, उनका नीर-क्षीर विवेक वह करता है, मानस पापों तक से दु:खी होता है।
महात्मा सूरदास जय परम भागवत हो रहे थे, तब उन्हें अपनी बुराइयाँ सूझीं। जब तक वे वस्तुत: पापी और व्यभिचारी रहे, तब तक उन्हें अपने काम में कोई बुराई न दीखी; पर जब वे भगवान् की शरण में आये तो भूतकाल की बुराइयों का स्मरण करने मात्र से उनकी आत्मा काँप गई और उसकी तीव्र संवेदना को शान्त करने के लिए अपने नेत्र फोड़ डाले। फिर भी आत्मनिरीक्षण करने पर उन्हें अपने भीतर दोष ही दोष दीखे, जिनकी घोषणा उन्होंने अपने प्रसिद्ध पद में की- ‘मो सम कौन कुटिल खल कामी।’
भुव: की भूमिका में पहुँचे हुए साधक के तीन लक्षण प्रधान रूप में होते हैं- (१) आत्मकल्याण के लिए तपश्चर्या में तीव्र प्रवृत्ति, (२) अपनी प्रगति को मन्द अनुभव करना, अपनी उन्नति के प्रति असन्तोष, (३) अपने विचार, कार्य एवं स्वभाव में अनेक बुराइयों का दिखाई देना। यह भूमिका धीरे-धीरे पकती रहती है। यदि हाँडी के भीतर शान्ति हो तो उसके दो कारण समझे जा सकते हैं- (१) या तो अभी पकना आरम्भ नहीं हुआ, हाँडी गरम नहीं हुई, (२) या पककर दाल बिलकुल तैयार हो गई। या तो अज्ञानान्धकार में डूबे हुए मूर्ख प्रकृति के लोग मुदित रहते हैं और अपनी बुराइयों में ही मौज करते हैं या फिर अन्तिम कक्षा में पहुँचा योगी आत्मसाक्षात्कार करके ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर शान्त हो जाता है। मध्यम कक्षा में तप, प्रयत्न, असन्तोष एवं वेदना की प्रधानता रहती है। यह स्थिति आवश्यक है, इसे ही आत्मा का अग्नि संस्कार कहते हैं। इसमें अन्त:करण का परिपाक होता है। शरीर को तपश्चर्याओं की अग्नि में और अन्त:करण को असन्तोष की अग्नि में तपाकर पकाया जाता है। पूरी मात्रा में अग्नि-संस्कार हो जाने पर न तो शरीर को तपाने की आवश्यकता रहती है और न ही मन को तपाना पड़ता है। तब वह तीसरी कक्षा ‘स्व:’ की शान्ति भूमिका प्राप्त करता है।
मन्त्र दीक्षा के लिये कोई भी विचारवान्, दूरदर्शी, उच्च चरित्र, प्रतिभाशाली सत्पुरुष उपयुक्त हो सकता है, वह अपनी तर्कशक्ति और बुद्धिमत्ता से शिष्य के विचारों का परिमार्जन कर सकता है। उसके कुविचारों को, भ्रमों को सुलझाकर अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक सलाह, शिक्षण एवं उपदेश दे सकता है, अपने प्रभाव से उसे प्रभावित भी कर सकता है। अग्नि दीक्षा के लिए ऐसा गुरु चाहिए जिसके भीतर अग्नि पर्याप्त मात्रा में हो, तप की पूँजी का धनी हो। दान वही कर सकता है जिसके पास धन हो, विद्या वही दे सकता है जिसके पास विद्या हो। जिसके पास जो वस्तु नहीं, वह दुसरों को क्या देगा? जिसने स्वयं तप करके प्राणशक्ति संचित की है, अग्नि अपने अन्दर प्रज्वलित कर रखी है, वही दूसरों को प्राण या अग्नि देकर भुव: भूमिका की दीक्षा दे सकता है।
तीसरी भूमिका ‘स्व:’ है। इसे ब्र्रह्म-दीक्षा कहते हैं। जब दूध अग्रि पर औटाकर नीचे अतार लिया जाता है और ठण्डा हो जाता है, तब उसमें दही का जामन देकर जमा दिया जाता है, फलस्वरुप वह सारा दही ही बन जाता है। मन्त्र द्वारा दृष्टिकोण का परिमार्जन करके साधक अपने सांसारिक जीवन को प्रसन्नता और सम्पन्नता से ओत-प्रोत करता है, अग्रि द्वारा अपने कुसंस्कारों, पापों, भूलों, कषायों, दुर्बलताओं को जलाता है, उनसे अपना पिण्ड छुड़ाकर बन्धन मुक्त होता है एवं तप की उष्मा द्वारा अन्त:करण को पकाकर ब्राह्मीभूत करता है। दूध पकते-पकते जब रबड़ी, मलाई आदि की शक्ल में पहुँच जाता है, तब उसका मूल्य और स्वाद बहुत बढ़ जाता है।
पहली ज्ञान-भूमि, दूसरी शक्ति-भूमि और तीसरी ब्रह्म-भूमि होती है। क्रमश: एक के बाद एक को पार करना पड़ता है। पिछली दो कक्षाओं को पार कर साधक जब तीसरी कक्षा में पहुँचता है, तो उसे सद्गुरु द्वारा ब्रह्म-दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। यह ‘परा’ वाणी द्वारा होती है। बैखरी वाणी द्वारा मुँह से शब्द उच्चारण करके ज्ञान दिया जाता है। मध्यमा और पश्यन्ती वाणियों द्वारा शिष्य के प्राणमय और मनोमय कोश में अग्रि संस्कार किया जाता है। परा वाणी द्वारा आत्मा बोलती है और उसका सन्देश दूसरी आत्मा सुनती है। जीभ की वाणी कान सुनते हैं, मन की वाणी नेत्र सुनते हैं, हृदय की वाणी हृदय सुनता है और आत्मा की वाणी आत्मा सुनती है। जीभ ‘बैखरी’ वाणी बोलती है, मन ‘मध्यमा’ बोलता है, हृदय की वाणी ‘पश्यन्ती’ कहलाती है और आत्मा ‘परा’ वाणी बोलती है। ब्रह्म-दीक्षा में जीभ, मन, हृदय किसी को नहीं बोलना पड़ता। आत्मा के अन्तरंग क्षेत्र में जो अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसेे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है। उसे ग्रहण करने के पश्चात् वह भी ऐसी ही ब्राह्मीभूत हो जाती है जैसा थोड़ा-सा दही पड़ने से औटाया हुआ दूध सबका सब दही बन जाता है।
काला कोयला या सड़ी-गली लकड़ी का टुकड़ा जब अग्नि में पड़ता है, तो उसका पुराना स्वरूप बदल जाता है और वह अग्निमय होकर अग्नि के ही गुणों से सुसज्जित हो जाता है। यह कोयला या लकड़ी का टुकड़ा भी अग्नि के गुणों से परिपूर्ण होता है और गर्मी, प्रकाश तथा जलाने की शक्ति भी उसमें अग्नि के समान होती है। ब्राह्मी दीक्षा से ब्रह्मभूत हुए साधक का शरीर तुच्छ होते हुए भी उसकी अन्तरंग सत्ता ब्राह्मीभूत हो जाती है। उसे अपने भीतर-बाहर चारों ओर सत् ही सत् दृष्टिगोचर होता है। विश्व में सर्वत्र उसे ब्रह्म ही ब्रह्म परिलक्षित होता है।
गीता में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट् रूप दिखाया था, अर्थात् उसे वह ज्ञान दिया था जिससे विश्व के अन्तरंग में छिपी हुई अदृश्य ब्रह्मसत्ता का दर्शन कर सके। भगवान् सब में व्यापक है, पर उसे कोई बिरले ही देखते, समझते हैं। भगवान् ने अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि दी जिससे उसकी ईक्षण शक्ति इतनी सूक्ष्म और पारदर्शी हो गयी कि वह उन दिव्य तत्वों का अनुभव करने लगा, जिसे साधारण लोग नहीं कर पाते। इस दिव्य दृष्टि को ही पाकर योगी लोग आत्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार अपने भीतर और बाहर करते हैं तथा ब्राह्मी गुणों से, विचारों से, स्वभावों से, कार्यों से ओतप्रोत हो जाते हैं। यशोदा ने, कौशल्या ने, काकभुशुण्डि ने ऐसी ही दिव्य दृष्टि पाई थी और ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। ईश्वर का दर्शन इसे ही कहते हैं। ब्रह्म दीक्षा पाने वाला शिष्य ईश्वर में अपनी समीपता और स्थिति का वैसे ही अनुभव करता है जैसे कोयला अग्रि में पड़कर अपने को अग्निमय अनुभव करता है।
द्विजत्व की तीन कक्षाएँ हैं-(१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य। पहली कक्षा है- वैश्य । वैश्य का उद्देश्य है- सुख सामग्री का उपार्जन। उसको मन्त्र (विचार) द्वारा यह लोक व्यवहार सिखाया जाता है, वह दृष्टिकोण दिया जाता है जिसके द्वारा सांसारिक जीवन सुखमय, शान्तिमय, सफल एवं सुसम्पन्न बन सके। बुरे गुण, कर्म एवं स्वभावों के कारण लोग अपने आपको चिन्ता, भय, दु:ख, रोग, क्लेश एवं दरिद्रता के चंगुल में फँसा लेते हैं। यदि उनका दृष्टिकोण सही हो, दस शूलों से बचे रहें तो निश्चय ही मानव जीवन स्वर्गीय आनन्द से ओत-प्रोत होना चाहिए।
क्षत्रिय तत्व का आधार है- शक्ति। शक्ति तप से उत्पन्न होती है। दो वस्तुओं को घिसने से गर्मी पैदा होती है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। बिजली की उत्पत्ति घर्षण से होती है। बुराइयों के, त्रुटियों के, कुसंस्कारों के, विकारों के विरुद्ध संघर्ष कार्य को तप कहते हैं। तप से आत्मिक शक्ति उत्पन्न होती है और उसे जिस दिशा में भी प्रयुक्त किया जाए उसी में चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं। शक्ति स्वयं ही चमत्कार है, शक्ति का नाम ही सिद्धि है। अग्रि-दीक्षा से तप आरम्भ होता है, आत्मदान के लिए युद्ध छेड़ा जाता है। गीता में भगवान् ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि ‘तू निरन्तर युद्ध कर।’ निरन्तर युद्ध किससे करता? महाभारत तो थोड़े ही दिन में समाप्त हो गया था, फिर अर्जुन निरन्तर किससे लड़ता? भगवान् का संकेत आन्तरिक शत्रुओं से संघर्ष जारी रखने का था। यही अग्रि-दीक्षा का उपदेश था। अग्नि-दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति में क्षत्रियत्व का, साहस का, शौर्य का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का विकास होता है। इससे वह यश का भागी बनता है।
मन्त्रदीक्षा से साधक व्यवहार कुशल बनता है और अपने जीवन को सुख-शांति, सहयोग एवं सम्पन्नता से भरा-पूरा कर लेता है। अग्रि-दीक्षा से उसकी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, ख्याति, प्रशंसा एवं महानता का प्रकाश होता है। दूसरों का सिर उसके चरणों में स्वत: झुक जाता है। लोग उसे नेता मानते हैं, उसका अनुसरण और अनुगमन करते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त दो दीक्षाओं द्वारा वैश्य और क्षत्रिय बनने के उपरान्त साधक ब्राह्मण बनने के लिए अग्रसर होता है। ब्रह्मदीक्षा से उसे ‘दिव्य दृष्टि’ मिलती है, इसे नेत्रोन्मीलन कहते हैं।
शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था। अर्जुन को भगवान् ने ‘‘दिव्यं ददामि ते चक्षु:’’ दिव्य नेत्र देकर अपने विराट् स्वरूप का दर्शन सम्भव करा दिया था। वह तृतीय नेत्र हर योगी का खुलता है, उसे वे बाते दिखाई पड़ती हैं जो साधारण व्यक्तियों को नहीं दिखतीं। उनको कण-कण में परमात्मा का पुण्य प्रकाश बहुमूल्य रत्नों की तरह जगमगाता हुआ दिखाई पड़ता है। भक्त माइकेल को प्रत्येक शिला में स्वर्गीय फरिश्ता दिखाई पड़ता था। सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि बड़ी संकुचित होती है, वे आज के हानि-लाभों में रोते-हँसते हैं, पर ब्रह्मज्ञानी दूर तक देखता है। वह वस्तु और परिस्थिति पर पारदर्शी विचार करता है और प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की लीला एवं दया का अनुभव करता हुआ प्रसन्न रहता है। विश्व मानव की सेवा में ही वह अपना जीवन लगाता है। इस प्रकार ब्रह्मदीक्षा में दीक्षित हुआ साधक परम भागवत होकर परम शान्ति को अन्त:करण में धारण करता हुआ दिव्य तत्वों से परिपूर्ण हो जाता है। इस श्रेणी के साधकों को ही भूसुर कहते हैं।
भुव: भूमिका में ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के चतुष्टय का संशोधन, परिमार्जन एवं विकास होता है। यह सब कार्य मध्यमा और पश्यन्ती वाणी द्वारा किया जाता है। वैखरी वाणी द्वारा वचनों के माध्यम से प्रारम्भिक साधक को ‘भू:’ क्षेत्र के मन्त्र दीक्षित को सलाह, शिक्षा आदि दी जाती है। जब प्राण दीक्षा होती है, तो गुरु अपना प्राण शिष्य के प्राण में घोल देता है, बीज रुप से अपना आत्मबल साधक के अन्त:करण में स्थापित कर देता है। जैसे आग से आग जलायी जाती है, बिजली की धारा से बल्व जलते या पंखे चलते हैं, उसी प्र्रकार अपना शक्ति-भाग बीज रूप से दूसरे की मनोभूमि में जमाकर वहाँ उसे सींचा और बढ़ाया जाता है। इस क्रिया पद्धति को अग्नि दीक्षा कहते हैं। अशक्त को सशक्त बनाना, निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराश को आशान्वित करना प्राण दीक्षा का काम है। मन से विचार उत्पन्न होता है, अग्नि से क्रिया उत्पन्न होती है। अन्त:भूमि में हलचल, क्रिया, प्रगति, चेष्टा, क्रान्ति, बेचैनी, आकांक्षा का तीव्र गति से उदय होता है।
साधारणत: लोग आत्मोन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं देते, थोड़ा-सा देते हैं तो उसे बड़ा भारी बोझ समझते हैं, कुछ जप तप करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है मानो बहुत बड़ा मोर्चा जीत रहे हों। परन्तु जब आन्तरिक स्थिति भुव: क्षेत्र में पहुँचती है, तो साधक को बड़ी बेचैनी और असन्तुष्टि होती है। उसे अपना साधन बहुत साधारण दिखाई पड़ता है और अपनी उन्नति उसे बहुत मामूली दीखती है। उसे छटपटाहट उवं जल्दी होती है कि मैं किस प्रकार शीघ्र लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। अपनी उन्नति चाहे कितनी ही सुव्यवस्थित ढंग से हो रही हो, पर उसे सन्तोष नहीं होता। यह व्याकुलता उसकी कोई भूल नहीं होती वरन् भीतर ही भीतर जो तीव्र क्रिया शक्ति काम कर रही है उसकी प्रतिक्रिया है। भीतरी क्रिया, प्रवृत्ति और प्रेरणा का बाह्य लक्षण असन्तोष है। यदि असन्तोष न हो, तो समझना चाहिए कि साधक की क्रिया शक्ति शिथिल हो गई। जो साधक दूसरी भूमिका में है, उसका असन्तोष जितना ही तीव्र होगा, उतनी ही क्रिया शक्ति तेजी से काम करती रहेगी। बुद्धिमान् पथ-प्रदर्शक दूसरी कक्षा के साधक में सदा असन्तोष भड़काने का प्रयत्न करते हैं ताकि आन्तरिक क्रिया और भी सतेज हो, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह असन्तोष कहीं निराशा में परिणत न हो जाय।
अग्नि दीक्षा लेकर साधक का आन्तरिक प्रकाश स्वच्छ हो जाता है और उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अँधेरे में, धुँधले प्रकाश में बड़ी वस्तुयें ही ठीक प्रकार दीखती हैं और कई बार तो प्रकाश की तेजी के कारण वे वस्तुएँ और भी अधिक महत्त्वपूर्ण दीखती हैं। आत्मा में ज्ञानाग्नि का प्रकाश होते ही साधक को अपनी छोटी-छोटी भूल, बुराई, कमियाँ भली प्रकार दीख पड़ती हैं। उसे मालूम पड़ता है कि मैं असंख्य बुराइयों का भण्डार हूँ, नीची श्रेणी के मनुष्यों से भी मेरी बुराइयाँ अधिक हैं। अब भी पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते। इस प्रकार वह अपने अन्दर घृणास्पद तत्त्वों को बड़ी मात्रा में देखता है। जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के लोग कतई गलती नहीं मानते, उनका नीर-क्षीर विवेक वह करता है, मानस पापों तक से दु:खी होता है।
महात्मा सूरदास जय परम भागवत हो रहे थे, तब उन्हें अपनी बुराइयाँ सूझीं। जब तक वे वस्तुत: पापी और व्यभिचारी रहे, तब तक उन्हें अपने काम में कोई बुराई न दीखी; पर जब वे भगवान् की शरण में आये तो भूतकाल की बुराइयों का स्मरण करने मात्र से उनकी आत्मा काँप गई और उसकी तीव्र संवेदना को शान्त करने के लिए अपने नेत्र फोड़ डाले। फिर भी आत्मनिरीक्षण करने पर उन्हें अपने भीतर दोष ही दोष दीखे, जिनकी घोषणा उन्होंने अपने प्रसिद्ध पद में की- ‘मो सम कौन कुटिल खल कामी।’
भुव: की भूमिका में पहुँचे हुए साधक के तीन लक्षण प्रधान रूप में होते हैं- (१) आत्मकल्याण के लिए तपश्चर्या में तीव्र प्रवृत्ति, (२) अपनी प्रगति को मन्द अनुभव करना, अपनी उन्नति के प्रति असन्तोष, (३) अपने विचार, कार्य एवं स्वभाव में अनेक बुराइयों का दिखाई देना। यह भूमिका धीरे-धीरे पकती रहती है। यदि हाँडी के भीतर शान्ति हो तो उसके दो कारण समझे जा सकते हैं- (१) या तो अभी पकना आरम्भ नहीं हुआ, हाँडी गरम नहीं हुई, (२) या पककर दाल बिलकुल तैयार हो गई। या तो अज्ञानान्धकार में डूबे हुए मूर्ख प्रकृति के लोग मुदित रहते हैं और अपनी बुराइयों में ही मौज करते हैं या फिर अन्तिम कक्षा में पहुँचा योगी आत्मसाक्षात्कार करके ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर शान्त हो जाता है। मध्यम कक्षा में तप, प्रयत्न, असन्तोष एवं वेदना की प्रधानता रहती है। यह स्थिति आवश्यक है, इसे ही आत्मा का अग्नि संस्कार कहते हैं। इसमें अन्त:करण का परिपाक होता है। शरीर को तपश्चर्याओं की अग्नि में और अन्त:करण को असन्तोष की अग्नि में तपाकर पकाया जाता है। पूरी मात्रा में अग्नि-संस्कार हो जाने पर न तो शरीर को तपाने की आवश्यकता रहती है और न ही मन को तपाना पड़ता है। तब वह तीसरी कक्षा ‘स्व:’ की शान्ति भूमिका प्राप्त करता है।
मन्त्र दीक्षा के लिये कोई भी विचारवान्, दूरदर्शी, उच्च चरित्र, प्रतिभाशाली सत्पुरुष उपयुक्त हो सकता है, वह अपनी तर्कशक्ति और बुद्धिमत्ता से शिष्य के विचारों का परिमार्जन कर सकता है। उसके कुविचारों को, भ्रमों को सुलझाकर अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक सलाह, शिक्षण एवं उपदेश दे सकता है, अपने प्रभाव से उसे प्रभावित भी कर सकता है। अग्नि दीक्षा के लिए ऐसा गुरु चाहिए जिसके भीतर अग्नि पर्याप्त मात्रा में हो, तप की पूँजी का धनी हो। दान वही कर सकता है जिसके पास धन हो, विद्या वही दे सकता है जिसके पास विद्या हो। जिसके पास जो वस्तु नहीं, वह दुसरों को क्या देगा? जिसने स्वयं तप करके प्राणशक्ति संचित की है, अग्नि अपने अन्दर प्रज्वलित कर रखी है, वही दूसरों को प्राण या अग्नि देकर भुव: भूमिका की दीक्षा दे सकता है।
तीसरी भूमिका ‘स्व:’ है। इसे ब्र्रह्म-दीक्षा कहते हैं। जब दूध अग्रि पर औटाकर नीचे अतार लिया जाता है और ठण्डा हो जाता है, तब उसमें दही का जामन देकर जमा दिया जाता है, फलस्वरुप वह सारा दही ही बन जाता है। मन्त्र द्वारा दृष्टिकोण का परिमार्जन करके साधक अपने सांसारिक जीवन को प्रसन्नता और सम्पन्नता से ओत-प्रोत करता है, अग्रि द्वारा अपने कुसंस्कारों, पापों, भूलों, कषायों, दुर्बलताओं को जलाता है, उनसे अपना पिण्ड छुड़ाकर बन्धन मुक्त होता है एवं तप की उष्मा द्वारा अन्त:करण को पकाकर ब्राह्मीभूत करता है। दूध पकते-पकते जब रबड़ी, मलाई आदि की शक्ल में पहुँच जाता है, तब उसका मूल्य और स्वाद बहुत बढ़ जाता है।
पहली ज्ञान-भूमि, दूसरी शक्ति-भूमि और तीसरी ब्रह्म-भूमि होती है। क्रमश: एक के बाद एक को पार करना पड़ता है। पिछली दो कक्षाओं को पार कर साधक जब तीसरी कक्षा में पहुँचता है, तो उसे सद्गुरु द्वारा ब्रह्म-दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। यह ‘परा’ वाणी द्वारा होती है। बैखरी वाणी द्वारा मुँह से शब्द उच्चारण करके ज्ञान दिया जाता है। मध्यमा और पश्यन्ती वाणियों द्वारा शिष्य के प्राणमय और मनोमय कोश में अग्रि संस्कार किया जाता है। परा वाणी द्वारा आत्मा बोलती है और उसका सन्देश दूसरी आत्मा सुनती है। जीभ की वाणी कान सुनते हैं, मन की वाणी नेत्र सुनते हैं, हृदय की वाणी हृदय सुनता है और आत्मा की वाणी आत्मा सुनती है। जीभ ‘बैखरी’ वाणी बोलती है, मन ‘मध्यमा’ बोलता है, हृदय की वाणी ‘पश्यन्ती’ कहलाती है और आत्मा ‘परा’ वाणी बोलती है। ब्रह्म-दीक्षा में जीभ, मन, हृदय किसी को नहीं बोलना पड़ता। आत्मा के अन्तरंग क्षेत्र में जो अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसेे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है। उसे ग्रहण करने के पश्चात् वह भी ऐसी ही ब्राह्मीभूत हो जाती है जैसा थोड़ा-सा दही पड़ने से औटाया हुआ दूध सबका सब दही बन जाता है।
काला कोयला या सड़ी-गली लकड़ी का टुकड़ा जब अग्नि में पड़ता है, तो उसका पुराना स्वरूप बदल जाता है और वह अग्निमय होकर अग्नि के ही गुणों से सुसज्जित हो जाता है। यह कोयला या लकड़ी का टुकड़ा भी अग्नि के गुणों से परिपूर्ण होता है और गर्मी, प्रकाश तथा जलाने की शक्ति भी उसमें अग्नि के समान होती है। ब्राह्मी दीक्षा से ब्रह्मभूत हुए साधक का शरीर तुच्छ होते हुए भी उसकी अन्तरंग सत्ता ब्राह्मीभूत हो जाती है। उसे अपने भीतर-बाहर चारों ओर सत् ही सत् दृष्टिगोचर होता है। विश्व में सर्वत्र उसे ब्रह्म ही ब्रह्म परिलक्षित होता है।
गीता में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट् रूप दिखाया था, अर्थात् उसे वह ज्ञान दिया था जिससे विश्व के अन्तरंग में छिपी हुई अदृश्य ब्रह्मसत्ता का दर्शन कर सके। भगवान् सब में व्यापक है, पर उसे कोई बिरले ही देखते, समझते हैं। भगवान् ने अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि दी जिससे उसकी ईक्षण शक्ति इतनी सूक्ष्म और पारदर्शी हो गयी कि वह उन दिव्य तत्वों का अनुभव करने लगा, जिसे साधारण लोग नहीं कर पाते। इस दिव्य दृष्टि को ही पाकर योगी लोग आत्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार अपने भीतर और बाहर करते हैं तथा ब्राह्मी गुणों से, विचारों से, स्वभावों से, कार्यों से ओतप्रोत हो जाते हैं। यशोदा ने, कौशल्या ने, काकभुशुण्डि ने ऐसी ही दिव्य दृष्टि पाई थी और ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। ईश्वर का दर्शन इसे ही कहते हैं। ब्रह्म दीक्षा पाने वाला शिष्य ईश्वर में अपनी समीपता और स्थिति का वैसे ही अनुभव करता है जैसे कोयला अग्रि में पड़कर अपने को अग्निमय अनुभव करता है।
द्विजत्व की तीन कक्षाएँ हैं-(१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य। पहली कक्षा है- वैश्य । वैश्य का उद्देश्य है- सुख सामग्री का उपार्जन। उसको मन्त्र (विचार) द्वारा यह लोक व्यवहार सिखाया जाता है, वह दृष्टिकोण दिया जाता है जिसके द्वारा सांसारिक जीवन सुखमय, शान्तिमय, सफल एवं सुसम्पन्न बन सके। बुरे गुण, कर्म एवं स्वभावों के कारण लोग अपने आपको चिन्ता, भय, दु:ख, रोग, क्लेश एवं दरिद्रता के चंगुल में फँसा लेते हैं। यदि उनका दृष्टिकोण सही हो, दस शूलों से बचे रहें तो निश्चय ही मानव जीवन स्वर्गीय आनन्द से ओत-प्रोत होना चाहिए।
क्षत्रिय तत्व का आधार है- शक्ति। शक्ति तप से उत्पन्न होती है। दो वस्तुओं को घिसने से गर्मी पैदा होती है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। बिजली की उत्पत्ति घर्षण से होती है। बुराइयों के, त्रुटियों के, कुसंस्कारों के, विकारों के विरुद्ध संघर्ष कार्य को तप कहते हैं। तप से आत्मिक शक्ति उत्पन्न होती है और उसे जिस दिशा में भी प्रयुक्त किया जाए उसी में चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं। शक्ति स्वयं ही चमत्कार है, शक्ति का नाम ही सिद्धि है। अग्रि-दीक्षा से तप आरम्भ होता है, आत्मदान के लिए युद्ध छेड़ा जाता है। गीता में भगवान् ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि ‘तू निरन्तर युद्ध कर।’ निरन्तर युद्ध किससे करता? महाभारत तो थोड़े ही दिन में समाप्त हो गया था, फिर अर्जुन निरन्तर किससे लड़ता? भगवान् का संकेत आन्तरिक शत्रुओं से संघर्ष जारी रखने का था। यही अग्रि-दीक्षा का उपदेश था। अग्नि-दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति में क्षत्रियत्व का, साहस का, शौर्य का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का विकास होता है। इससे वह यश का भागी बनता है।
मन्त्रदीक्षा से साधक व्यवहार कुशल बनता है और अपने जीवन को सुख-शांति, सहयोग एवं सम्पन्नता से भरा-पूरा कर लेता है। अग्रि-दीक्षा से उसकी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, ख्याति, प्रशंसा एवं महानता का प्रकाश होता है। दूसरों का सिर उसके चरणों में स्वत: झुक जाता है। लोग उसे नेता मानते हैं, उसका अनुसरण और अनुगमन करते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त दो दीक्षाओं द्वारा वैश्य और क्षत्रिय बनने के उपरान्त साधक ब्राह्मण बनने के लिए अग्रसर होता है। ब्रह्मदीक्षा से उसे ‘दिव्य दृष्टि’ मिलती है, इसे नेत्रोन्मीलन कहते हैं।
शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था। अर्जुन को भगवान् ने ‘‘दिव्यं ददामि ते चक्षु:’’ दिव्य नेत्र देकर अपने विराट् स्वरूप का दर्शन सम्भव करा दिया था। वह तृतीय नेत्र हर योगी का खुलता है, उसे वे बाते दिखाई पड़ती हैं जो साधारण व्यक्तियों को नहीं दिखतीं। उनको कण-कण में परमात्मा का पुण्य प्रकाश बहुमूल्य रत्नों की तरह जगमगाता हुआ दिखाई पड़ता है। भक्त माइकेल को प्रत्येक शिला में स्वर्गीय फरिश्ता दिखाई पड़ता था। सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि बड़ी संकुचित होती है, वे आज के हानि-लाभों में रोते-हँसते हैं, पर ब्रह्मज्ञानी दूर तक देखता है। वह वस्तु और परिस्थिति पर पारदर्शी विचार करता है और प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की लीला एवं दया का अनुभव करता हुआ प्रसन्न रहता है। विश्व मानव की सेवा में ही वह अपना जीवन लगाता है। इस प्रकार ब्रह्मदीक्षा में दीक्षित हुआ साधक परम भागवत होकर परम शान्ति को अन्त:करण में धारण करता हुआ दिव्य तत्वों से परिपूर्ण हो जाता है। इस श्रेणी के साधकों को ही भूसुर कहते हैं।
Versions
-

ENGLISHSuper Science of GayatriScan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानScan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 1Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 2Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 3Scan Book Version
-
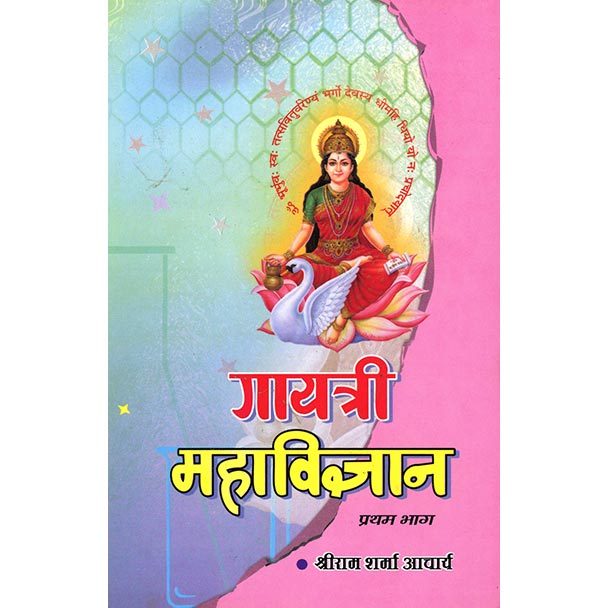
MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग १Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग २Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग ३Scan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानText Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग)Text Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान भाग 2Text Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री महाविज्ञान भाग १
- वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति
- ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव
- गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है
- गायत्री साधना से शक्तिकोशों का उद्भव
- शरीर में गायत्री मंत्र के अक्षर
- गायत्री और ब्रह्म की एकता
- महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान
- त्रिविध दु:खों का निवारण
- गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना
- गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता
- गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण
- जीवन का कायाकल्प
- नारियों को वेद एवं गायत्री का अधिकार
- देवियों की गायत्री साधना
- गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य
- गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत (जनेऊ)
- साधकों के लिये उपवीत आवश्यक है
- गायत्री साधना का उद्देश्य
- निष्काम साधना का तत्त्व ज्ञान
- गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध
- साधना- एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- आत्मशक्ति का अकूत भण्डार :: अनुष्ठान
- सदैव शुभ गायत्री यज्ञ
- महिलाओं के लिये विशेष साधनाएँ
- एक वर्ष की उद्यापन साधना
- गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि
- गायत्री का अर्थ चिन्तन
- साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते
- साधना की सफलता के लक्षण
- सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिये
- गायत्री द्वारा कुण्डलिनी जागरण
- यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बाँटिये
- गायत्री महाविज्ञान भाग ३ भूमिका
- गायत्री के पाँच मुख
- अनन्त आनन्द की साधना
- गायत्री मञ्जरी
- अन्नमय कोश और उसकी साधना
- उपवास - अन्नमय कोश की साधना
- आसन - अन्नमय कोश की साधना
- तत्त्व शुद्धि - अन्नमय कोश की साधना
- तपश्चर्या - अन्नमय कोश की साधना
- मनोमय कोश की साधना
- ध्यान - मनोमय कोश की साधना
- त्राटक - मनोमय कोश की साधना
- जप - मनोमय कोश की साधना
- तन्मात्रा साधना - मनोमय कोश की साधना
- विज्ञानमय कोश की साधना
- सोऽहं साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मानुभूति योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मचिन्तन की साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- स्वर योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- वायु साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- ग्रन्थि-भेद - विज्ञानमय कोश की साधना
- आनन्दमय कोश की साधना
- नाद साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- बिन्दु साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- कला साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- तुरीयावस्था - आनन्दमय कोश की साधना
- पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य
- गायत्री-साधना निष्फल नहीं जाती
- पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य
- गायत्री का तन्त्रोक्त वाम-मार्ग
- गायत्री की गुरु दीक्षा
- आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- मन्त्र दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- अग्नि दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्म दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- कल्याण मन्दिर का प्रवेश द्वार - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्मदीक्षा की दक्षिणा आत्मदान - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- वर्तमानकालीन कठिनाइयाँ - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ

