गायत्री महाविज्ञान 
पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
Read Scan Version
अग्रि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल, बदल या गल जाते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्रि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन न होता हो। तपस्या की अग्रि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मनभावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है।
पापों का गलना— जो प्रारब्ध- कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवितव्यता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भाँति सुनिश्चित हो चुका है, वे कष्टसाध्य भोग तपस्या की अग्रि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं, उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम दो महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर दो महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की सम्भावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से दस- बीस बूँद खून बहकर निवृत्त हो जाता है। जन्म- जन्मान्तरों के संचित वे पाप जो कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी- थोड़ी चिह्नपूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग, मुक्ति का अत्यन्त वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्राय: कुछ असुविधाएँ रहती हैं। इसका कारण यह है कि जन्म- जन्मान्तरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए, इसलिये ईश्वरीय वरदान की तरह हलके- फुलके कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों का गलना हुआ।
पापों का बदलना— यह इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश, कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसवकाल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ- साथ एक उल्लास भी रहता है। चन्द्र- से मुख का सुन्दर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिलकुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चन्द्र, दधीचि, प्रह्लाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, उनके लिये उस काल में भी वे उल्लासमय थे। अन्तत: अमर कीर्ति और सद्गति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिये सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तप द्वारा इस प्रकार ‘उधार पट जाना और मेहमान जीम जाना’ दो कार्य एक साथ हो जाते हैं।
पापों का जलना- पापों का जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे- मोटे अशुभ कर्म तप की अग्रि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घात- पात के ढेर को अग्रि की छोटी- सी चिनगारी जला डालती है, वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म तपश्चर्या, प्रायश्चित्त और भविष्य में वैसा न करने के दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अन्धकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अन्त:करण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गन्ध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अन्त हो जाता है।
तपश्चर्या से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो- सो बात ही नहीं है, वरन् तपस्वी में एक नयी परम सात्त्विक अग्रि पैदा होती है। इस अग्रि को दैवी विद्युत् शक्ति, आत्मतेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अन्त:करण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जाग्रत् होती हैं, दिव्य सद्गुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिये तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देव- दानवों ने तपस्याएँ करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाये हैं।
घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से चौदह रत्न मिले। दूध के मथने से घी निकलता है। काम- मन्थन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि- मन्थन से अन्न उपजता है। तपस्या द्वारा आत्ममन्थन से उच्च आध्यात्मिक तत्त्वों की वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। अग्रि में तपाने से सोना निर्मल बनता है। तप से तपा हुआ मनुष्य भी पापमुक्त, तेजस्वी और विवेकवान् बन जाता है।
अपनी तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। नीचे कुछ पापनाशिनी और ब्रह्मतेज- वद्र्धिनी तपश्चर्याएँ बताई जाती हैं—
अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिये भगवान् को युग- युग में अवतार लेकर अगणित हत्यायें करनी पड़ती हैं और रक्त की धार बहानी पड़ती है। इसमें पाप नहीं होता। सदुद्देश्य के लिये किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किये गये, सताये गये, बुभुक्षित, सन्त्रस्त, दु:खी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों, अज्ञानी बालक, रोगी अथवा पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो वह क्षम्य माने जाते हैं; कारण यह है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता।
पापियों की सूची में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं, जिन्हें उपर्युक्त किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े, पीछे वे उनके स्वभाव में आ गये। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गये। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियाँ, सुविधायें उन्हें मिलतीं, ऊँचा उठाने वाले और सन्तोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चय ही वे अच्छे बने होते।
कानून और लोकमत चाहे किसी को कितना ही दोषी ठहरा सकता है, स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यन्त बुरा हो सकता है, पर वास्तविक पापियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। जो परिस्थितियों के वश बुरे बन गये हैं, उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण तत्त्वत: पवित्र है। बुराई उसके ऊपर छाया मैल है। मैल को साफ करना न तो असम्भव है और न कष्टसाध्य, वरन् यह कार्य आसानी से हो सकता है।
पापों का गलना— जो प्रारब्ध- कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवितव्यता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भाँति सुनिश्चित हो चुका है, वे कष्टसाध्य भोग तपस्या की अग्रि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं, उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम दो महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर दो महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की सम्भावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से दस- बीस बूँद खून बहकर निवृत्त हो जाता है। जन्म- जन्मान्तरों के संचित वे पाप जो कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी- थोड़ी चिह्नपूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग, मुक्ति का अत्यन्त वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्राय: कुछ असुविधाएँ रहती हैं। इसका कारण यह है कि जन्म- जन्मान्तरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए, इसलिये ईश्वरीय वरदान की तरह हलके- फुलके कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों का गलना हुआ।
पापों का बदलना— यह इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश, कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसवकाल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ- साथ एक उल्लास भी रहता है। चन्द्र- से मुख का सुन्दर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिलकुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चन्द्र, दधीचि, प्रह्लाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, उनके लिये उस काल में भी वे उल्लासमय थे। अन्तत: अमर कीर्ति और सद्गति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिये सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तप द्वारा इस प्रकार ‘उधार पट जाना और मेहमान जीम जाना’ दो कार्य एक साथ हो जाते हैं।
पापों का जलना- पापों का जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे- मोटे अशुभ कर्म तप की अग्रि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घात- पात के ढेर को अग्रि की छोटी- सी चिनगारी जला डालती है, वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म तपश्चर्या, प्रायश्चित्त और भविष्य में वैसा न करने के दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अन्धकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अन्त:करण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गन्ध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अन्त हो जाता है।
तपश्चर्या से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो- सो बात ही नहीं है, वरन् तपस्वी में एक नयी परम सात्त्विक अग्रि पैदा होती है। इस अग्रि को दैवी विद्युत् शक्ति, आत्मतेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अन्त:करण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जाग्रत् होती हैं, दिव्य सद्गुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिये तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देव- दानवों ने तपस्याएँ करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाये हैं।
घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से चौदह रत्न मिले। दूध के मथने से घी निकलता है। काम- मन्थन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि- मन्थन से अन्न उपजता है। तपस्या द्वारा आत्ममन्थन से उच्च आध्यात्मिक तत्त्वों की वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। अग्रि में तपाने से सोना निर्मल बनता है। तप से तपा हुआ मनुष्य भी पापमुक्त, तेजस्वी और विवेकवान् बन जाता है।
अपनी तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। नीचे कुछ पापनाशिनी और ब्रह्मतेज- वद्र्धिनी तपश्चर्याएँ बताई जाती हैं—
(१) अस्वाद तप
तप उन कष्टों को कहते हैं, जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा ये दो स्वाद की प्रधान वस्तुएँ हैं। इनमें से एक भी वस्तु न डाली जाए, तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। प्राय: लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्त्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है, उसे सात्त्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। राजसिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे- जैसे स्वाद रहित भोजन में सन्तोष पैदा होता है, वैसे ही वैसे सात्त्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारम्भ में एक सप्ताह, एक मास या एक ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिये। आरम्भ में बहुत लम्बे समय के लिये नहीं करना चाहिये। यह अस्वाद- तप हुआ।
(२) तितिक्षा तप
सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है, उसे थोड़ा- थोड़ा सहन करना चाहिये। जाड़े की की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता दो वस्त्रों में गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा ओढक़र या कम्बल से काम चलाना, गरम पानी का प्रयोग न करके ताजे जल से स्नान करना, अग्रि न तापना, यह शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग यह गर्मी की तपश्चर्या है।
(३) कर्षण तप
प्रात:काल एक- दो घण्टे रात रहे उठकर नित्यकर्म में लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिये स्वयं जल भरकर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपनी सेवा के काम दूसरों से कम से कम कराना, जूता न पहनकर खड़ाऊ या चट्टी से काम चलाना, पलग पर शयन न करके तख्त या भूमि पर शयन करना, धातु के बर्तन प्रयोग न करके पत्तल या हाथ में भोजन करना, पशुओं की सवारी न करना, खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप हैं। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है।
(४) उपवास
गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरम्भिक उपवास है। धीरे- धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिये। दो समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के पीना चाहिये। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं, वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्रि आँतों में पड़े मल को सुखाकर गाँठें बना देती है, इसलिये उपवास में कई बार पानी पीना चाहिये। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए, तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है।
(५) गव्यकल्प तप
शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिये गव्यकल्प अभूतपूर्व तप है। राजा दिलीप जब निस्सन्तान रहे, तो उन्होंने कुलगुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नन्दिनी गौ को वे चराते थे और गोरस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन करना, गाय के गोबर के कण्डों से दूध गरम करना चाहिये। गोमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्मरोगों तथा रक्तविकारों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्त्विक एवं बलदायक होता है, इसलिये गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य तीन मास निर्वाह करे, तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है।
(६) प्रदातव्य तप
अपने पास जो शक्ति हो, उसमें से कम मात्रा में अपने लिये रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना प्रदातव्य तप है। धनी आदमी धन का दान करते हैं। जो धनी नहीं हैं, वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि का उधार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन- दान की ही भाँति महत्त्वपूर्ण है। अनीति उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित्त यही है कि उसको सत्कार्य के लिये दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोकसेवा के लिये लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान रखना आवश्यक है। कुपात्र को दिया हुआ, अनुपयुक्त कर्म के लिये दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्येतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिडिय़ाँ, कुत्ते आदि उपकारी जीव- जन्तुओं को भी अन्न- जल का दान देने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये।
स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्त्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान की प्रशंसा में धर्मशास्त्रों का पन्ना- पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के सम्बन्ध में अधिक क्या कहा जाए! वेद ने कहा है- ‘‘सौ हाथों से कमाये और हजार हाथों से दान करे।’’
(७) निष्कासन तप
अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं; वैसे ही अपने पापों को छुपाकर रखा जाए, तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गन्दगी और सडऩ पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिये कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिये जो काफी गम्भीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप- कथाएँ कह देनी चाहिये। अपनी कठिनाइयाँ, दु:ख- गाथाएँ, इच्छाएँ, अनुभूतियाँ भी इसी प्रकार किन्हीं ऐसे लोगों से क हते रहना चाहिए, जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा न करें और कभी विरोधी हो जाने पर भी उन्हें दूसरों से प्रकट करके हानि न पहुँचाएँ। यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है, जिससे मनोभूमि निर्मल होती है।
प्रायश्चित्तों में ‘दोष प्रकाशन’ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गो- हत्या हो जाने का प्रायश्चित्त शास्त्रों ने यह बताया है कि मरी गौ की पूँछ हाथ में लेकर एक सौ गाँवों में वह व्यक्ति उच्च स्वर से चिल्ला- चिल्लाकर यह कहे कि मुझसे गौ- हत्या हो गयी। इस दोष प्रकाशन से गौ- हत्या का दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो, उससे क्षमा माँगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वह सन्तुष्ट हो सके वह करना चाहिए। यदि वह भी न हो, तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अन्तरात्मा का एक भारी बोझ तो हलका करना ही चाहिए। इस प्रकार के दोष प्रकाशन के लिये ‘शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार’ को एक विश्वसनीय मित्र समझकर पत्र द्वारा अपने दोषों को लिखकर उनके प्रायश्चित्त तथा सुधार की सलाह प्रसन्नतापूर्वक ली जा सकती है।
(८) साधना तप
गायत्री का चौबीस हजार जप नौ दिन में पूरा करना, सवालक्ष जप चालीस दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएँ, पुरश्चरण, पूजन, स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग ‘गायत्री चालीसा’ का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामन्त्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं।
(९) ब्रह्मचर्य तप
वीर्य- रक्षा, मैथुन से बचना, काम- विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम- सेवन शारीरिक काम- सेवन की ही भाँति हानिकारक है। मन को कामक्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाये रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में, सत् तत्त्व में लगाये रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर्य रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से तीन लाभ करने वाला यह तप गायत्री साधना वालों के लिये सब प्रकार उत्तम है।
(१०) चान्द्रायण तप
यह व्रत पूर्णमासी से आरम्भ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खूराक हो, उसका चौदहवाँ भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिये। कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा जैसे १- १ कला नित्य घटता है, वैसे ही १- १ चतुर्दशांश नित्य कम करते चलना चाहिये। अमावस्या और प्रतिपदा को चन्द्रमा बिलकुल दिखाई नहीं पड़ता। उन दो दिनों बिलकुल भी आहार न लेना चाहिये। फिर शुक्ल पक्ष की दूज को चन्द्रमा एक कला से निकलता है और धीरे- धीरे बढ़ता है, वैसे ही १- १ चतुर्दशांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुँच जाना चाहिये। एक मास में आहार- विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्त्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न रहना चाहिये।
अर्ध चान्द्रायण व्रत पन्द्रह दिन का होता है। उसमें भोजन का सातवाँ भाग सात दिन कम करना और सात दिन बढ़ाना होता है। बीच का एक दिन निराहार रहने का होता है। आरम्भ में अर्ध चान्द्रायण ही करना चाहिये। जब एक बार सफलता मिल जाए, तो पूर्ण चान्द्रायण के लिये कदम बढ़ाना चाहिये।
उपवास स्वास्थ्यरक्षा का बड़ा प्रभावशाली साधन है। मनुष्य से खान- पान में जो त्रुटियाँ स्वभाव या परिस्थितिवश होती रहती हैं, उनसे शरीर में दूषित या विजातीय तत्त्व की वृद्धि हो जाती है। उपवास काल में जब पेट खाली रहता है, तो जठराग्रि उन दोषों को ही पचाने लगती है। इसमें शरीर शुद्ध होता है और रक्त स्वच्छ हो जाता है। जिसकी देह में विजातीय तत्त्व नहीं होंगे और नाडिय़ों में स्वच्छ रक्त परिभ्रमण करता होगा, उसको एकाएक किसी रोग या बीमारी की शिकायत हो ही नहीं सकती ।। इसलिये स्वास्थ्यकामी पुरुष के लिये उपवास बहुत बड़े सहायक बन्धु के समान है। अन्य उपवासों से चान्द्रायण व्रत में यह विशेषता है कि इसमें भोजन का घटाना और बढ़ाना एक नियम और क्रम से होता है, जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता। अन्य लम्बे उपवासों में जिनमें भोजन को लगातार दस- पन्द्रह दिन के लिये छोड़ दिया जाता है, उपवास को खत्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और अधिकांश व्यक्ति उस समय अधिक मात्रा में अनुपयुक्त आहार कर लेने से कठिन रोगों के शिकार हो जाते हैं। यह चान्द्रायण व्रत में बिलकुल नहीं होता।
(११) मौन तप
मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, दैवी तत्त्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शान्ति का प्रादुर्भाव होता है, बहिर्मुखी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिये निश्चित करना चाहिये। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन अवधि निर्धारित करनी चाहिये। मौन काल का अधिकांश भाग एकान्त में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिन्तन में व्यतीत करना चाहिये।
(१२) अर्जन तप
विद्याध्ययन, शिल्प- शिक्षा, देशाटन, मल्ल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थी को जिस प्रकार कष्ट उठाना पड़ता है, मन मारना पड़ता है और सुविधाएँ छोडक़र कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यन्त किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। साल में थोड़ा- सा समय तो इस तपस्या में लगाना ही चाहिये, जिससे अपनी तपस्याएँ बढ़ती चलें और उनके द्वारा अधिक लोक- सेवा करना सम्भव हो सके।
सूर्य की बारह राशियाँ होती हैं, गायत्री के वह बारह तप हैं। इनमें से जो तप, जब, जिस प्रकार सम्भव हो, उसे अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिये। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के बारह महीनों में एक- एक महीने एक- एक तप करके एक वर्ष पूरा ‘तप- वर्ष’ बिताया जाए। सातवें निष्कासन तप में एक- दो बार विश्वस्त मित्रों के सामने दोष प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में एक मास तक अपनी बुराइयाँ लिखते रहना चाहिये और उन्हें अपने पथ- प्रदर्शक को दिखाना चाहिये। यह क्रम अधिक दिन तक चालू रखा जाए तो और भी उत्तम है। महात्मा गाँधी साबरमती आश्रम में अपने आश्रमवासियों की डायरी बड़े गौर से जाँचा करते थे।
अन्य तपों में प्रत्येक को प्रयोग करने के लिये अनेकों रीतियाँ हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी- थोड़ी अवधि के लिये निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिये। आरम्भ में थोड़ा और सरल तप अपनाने से पीछे दीर्घकाल तक और कठिन स्वाध्याय साधन करना भी सुलभ हो जाता है।
गायत्री साधना से पापमुक्ति
गायत्री की अनन्त कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्त्व पर विचार करते हुए हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत काँच या पारदर्शी पात्र में किसी रंग का पानी भर दिया जाए, तो उसी रंग का दीखने लगेगा, साधारणत: उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी भर दिया जाए, तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्मा स्वभावत: निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव भर जाते हैं, वह उसी प्रकार का दिखाई देने लगता है।
गीता में कहा है कि- ‘‘विद्या सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल आदि को जो समत्व बुद्धि से देखता है, वही पण्डित है।’’ इस समन्वय का रहस्य यह है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है, उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार अन्त:करण चतुष्टय रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक, विपन्न, विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए, तो आज के दुष्ट का कल ही सन्त बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास बताता है कि एक चाण्डाल कुलोत्पन्न तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया। जीवन भर वेश्यावृत्ति करने वाली गणिका आन्तरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी देवियों को प्राप्त होने वाली परमगति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पेशा करते हुए जिन्दगी गुजार देने वाले अजामिल और सदन परम भागवत भक्त कहलाए। इस प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले उच्चता को प्राप्त हुए हैं और हीन कुलोत्पन्नों को उच्च वर्ण की प्रतिष्ठा मिली है। रैदास चमार, कबीर जुलाहे, रामानुज शूद्र, षट्कोपाचार्य खटीक, तिरवल्लुवर अन्त्यज वर्ण में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊँची थी। विश्वामित्र भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे।
जहाँ पतित स्थान से ऊपर चढऩे के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, वहाँ उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम नहीं हैं। पुलस्त्य के उत्तम ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का महापण्डित रावण, मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष, अन्यायी कौरवों के समर्थक हो गये। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वसिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पाराशर ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके सन्तान उत्पन्न की। विश्वामित्र ने वेश्या पर आसक्त होकर उसे लम्बे समय तक अपने पास रखा। चन्द्रमा जैसा देवता गुरुमाता के साथ कुमार्गगामी बना। देवताओं के राजा इन्द्र को व्यभिचार के कारण शाप का भाजन होना पड़ा। ब्रह्म अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गये। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करने स्वयंवर में जा पहुँचे। सड़ी- गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलि राजा के दान में भाँजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी एक आँख गँवा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर कालिख पोती और धीरे से ‘नरो वा कुंजरो वा’ गुनगुनाकर अपने को झूठ से बचाने की प्रवञ्चना की। कहाँ तक कहें! किस- किस की कहें! इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़ों- बड़ों को स्थानच्युत हुआ पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि आन्तरिक स्थिति में हेर- फेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन सकते हैं।
शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं। पीछे संस्कार के प्रभाव से द्विज बनते हैं। असल में यह संस्कार ही है, जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बना देते हैं। गायत्री के तत्त्वज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है, जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है।
पापों का नाश आत्मतेज की प्रचण्डता से होता है। यह तेजी जितनी अधिक होती है, उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र और अधिक परिमाण में होता है। बिना धार की लोहे की छड़ से वह कार्य नहीं हो सकता, जो तीक्ष्ण तलवार से होता है। यह तेजी किस प्रकार आए? इसका उपाय तपाना और रगडऩा है। लोहे को आग में तपाकर उसमें धार बनाई जाती है और पत्थर पर रगडक़र उसे तेज किया जाता है। तब वह तलवार दुश्मन की सेना का सफाया करने योग्य होती है। हमें भी अपनी आत्मशक्ति तेज करने के लिये इसी तपाने, घिसने वाली प्रणाली को अपनाना पड़ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में ‘तप’ या ‘प्रायश्चित्त’ नाम से पुकारते हैं।
प्रायश्चित्त क्यों? कैसे?— अपराधों की निवृत्ति के लिये हर जगह दण्ड का विधान काम में लाया जाता है। बच्चे ने गड़बड़ी की कि माता की डाँट- डपट पड़ी। शिष्य ने प्रमाद किया कि गुरु ने छड़ी सँभाली। सामाजिक नियमों को भंग किया कि पंचायत ने दण्ड दिया। कानून का उल्लंघन हुआ कि जुर्माना, जेल, कालापानी या फाँसी तैयार है। ईश्वर दैविक, दैहिक, भौतिक दु:ख देकर पापों का दण्ड देता है। दण्ड विधान प्रतिशोध या प्रतिहिंसा मात्र नहीं है। ‘खून का बदला खून’ की जंगली प्रथा के कारण नहीं, दण्ड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर किया गया है। कारण यह है कि दण्ड स्वरूप जो कष्ट दिये जाते हैं, उनसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और भूल को छोडक़र उचित मार्ग पर आ जाता है। तप में ऐसी शक्ति है। तप की गर्मी से अनात्म तत्त्वों का संहार होता है।
दूसरों द्वारा दण्ड रूप में बलात् तप कराके हमारी शुद्धि की जाती है। उस प्रणाली को हम स्वयं ही अपनाएँ, अपने गुप्त- प्रकट पापों का दण्ड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छापूर्वक तप करें, तो वह दूसरों द्वारा बलात् कराये हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम है। उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा एवं न आत्मग्लानि से चित्त क्षोभित होता है, वरन् स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनन्द आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिये आत्मतेज की अग्रि चाहिए। इस अग्रि की उत्पत्ति से दुहरा लाभ होता है, एक तो हानिकारक तत्त्वों का, कषाय- कल्मषों का नाश होता है, दूसरे उनकी ऊष्मा और प्रकाश से दैवी तत्त्वों का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में पग- पग पर व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचरण- विचार आदि के विधि- विधान इसी दृष्टि से किये गये हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दुहरे लाभों को उठा सके।
‘अपने से कोई भूल, पाप या बुराइयाँ बन पड़ी हों, तो उनके अशुभ फलों के निवारण के लिये सच्चा प्रायश्चित्त तो यही है कि उन्हें फिर न करने का दृढ़ निश्चय किया जाए, पर यदि इस निश्चय के साथ- साथ थोड़ी तपश्चर्या भी की जाए, तो उसे प्रतिज्ञा का बल मिलता है और उसके पालन में दृढ़ता आती है। साथ ही यह तपश्चर्या सात्त्विकता की तीव्रगति से वृद्धि करती है, चैतन्यता उत्पन्न करती है और ऐसे उत्तमोत्तम गुण, कर्म, स्वभावों को उत्पन्न करती है, जिनसे पवित्रतामय, साधनामय, मंगलमय जीवन बिताना सुगम हो जाता है। गायत्री शक्ति के आधार पर की गयी तपश्चर्या बड़े- बड़े पापियों को भी निष्पाप बनाने, उनके पाप- पुंजों को नष्ट करने तथा भविष्य के लिये उन्हें निष्पाप रहने योग्य बना सकती है।’
क्रिया नहीं, भाव प्रधान—जो कार्य पाप दिखाई पड़ते हैं, वे सर्वदा वैसे पाप नहीं होते जैसे कि समझते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य न तो पाप है न पुण्य; कर्ता की भावना के अनुसार पाप- पुण्य होते हैं। जो कार्य एक मनुष्य के लिये पाप है, वही दूसरे के लिए पापरहित है और किसी के लिये वह पुण्य भी है। हत्या करना एक कर्म है, वह तीन व्यक्तियों के लिये तीन विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिये किसी की हत्या करता है, यह हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिये प्राणदण्ड देता है, वह उसके लिये कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आततायी डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिये अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है, तो वह पुण्य है। हत्या तीनों ने ही की, पर तीनों की हत्यायें अलग- अलग परिणाम वाली हैं। तीनों हत्यारे डाकू, न्यायाधीश एवं आततायी से लड़कर उसका वध करने वाले- समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते ।।
चोरी एक बुरा कार्य है, परन्तु परिस्थितियों वश वह भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं सम्पन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है, वह पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण लीजिये- भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी सम्पन्न व्यक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है।
तप उन कष्टों को कहते हैं, जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा ये दो स्वाद की प्रधान वस्तुएँ हैं। इनमें से एक भी वस्तु न डाली जाए, तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। प्राय: लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्त्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है, उसे सात्त्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। राजसिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे- जैसे स्वाद रहित भोजन में सन्तोष पैदा होता है, वैसे ही वैसे सात्त्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारम्भ में एक सप्ताह, एक मास या एक ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिये। आरम्भ में बहुत लम्बे समय के लिये नहीं करना चाहिये। यह अस्वाद- तप हुआ।
(२) तितिक्षा तप
सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है, उसे थोड़ा- थोड़ा सहन करना चाहिये। जाड़े की की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता दो वस्त्रों में गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा ओढक़र या कम्बल से काम चलाना, गरम पानी का प्रयोग न करके ताजे जल से स्नान करना, अग्रि न तापना, यह शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग यह गर्मी की तपश्चर्या है।
(३) कर्षण तप
प्रात:काल एक- दो घण्टे रात रहे उठकर नित्यकर्म में लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिये स्वयं जल भरकर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपनी सेवा के काम दूसरों से कम से कम कराना, जूता न पहनकर खड़ाऊ या चट्टी से काम चलाना, पलग पर शयन न करके तख्त या भूमि पर शयन करना, धातु के बर्तन प्रयोग न करके पत्तल या हाथ में भोजन करना, पशुओं की सवारी न करना, खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप हैं। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है।
(४) उपवास
गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरम्भिक उपवास है। धीरे- धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिये। दो समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के पीना चाहिये। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं, वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्रि आँतों में पड़े मल को सुखाकर गाँठें बना देती है, इसलिये उपवास में कई बार पानी पीना चाहिये। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए, तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है।
(५) गव्यकल्प तप
शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिये गव्यकल्प अभूतपूर्व तप है। राजा दिलीप जब निस्सन्तान रहे, तो उन्होंने कुलगुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नन्दिनी गौ को वे चराते थे और गोरस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन करना, गाय के गोबर के कण्डों से दूध गरम करना चाहिये। गोमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्मरोगों तथा रक्तविकारों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्त्विक एवं बलदायक होता है, इसलिये गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य तीन मास निर्वाह करे, तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है।
(६) प्रदातव्य तप
अपने पास जो शक्ति हो, उसमें से कम मात्रा में अपने लिये रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना प्रदातव्य तप है। धनी आदमी धन का दान करते हैं। जो धनी नहीं हैं, वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि का उधार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन- दान की ही भाँति महत्त्वपूर्ण है। अनीति उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित्त यही है कि उसको सत्कार्य के लिये दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोकसेवा के लिये लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान रखना आवश्यक है। कुपात्र को दिया हुआ, अनुपयुक्त कर्म के लिये दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्येतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिडिय़ाँ, कुत्ते आदि उपकारी जीव- जन्तुओं को भी अन्न- जल का दान देने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये।
स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्त्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान की प्रशंसा में धर्मशास्त्रों का पन्ना- पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के सम्बन्ध में अधिक क्या कहा जाए! वेद ने कहा है- ‘‘सौ हाथों से कमाये और हजार हाथों से दान करे।’’
(७) निष्कासन तप
अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं; वैसे ही अपने पापों को छुपाकर रखा जाए, तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गन्दगी और सडऩ पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिये कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिये जो काफी गम्भीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप- कथाएँ कह देनी चाहिये। अपनी कठिनाइयाँ, दु:ख- गाथाएँ, इच्छाएँ, अनुभूतियाँ भी इसी प्रकार किन्हीं ऐसे लोगों से क हते रहना चाहिए, जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा न करें और कभी विरोधी हो जाने पर भी उन्हें दूसरों से प्रकट करके हानि न पहुँचाएँ। यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है, जिससे मनोभूमि निर्मल होती है।
प्रायश्चित्तों में ‘दोष प्रकाशन’ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गो- हत्या हो जाने का प्रायश्चित्त शास्त्रों ने यह बताया है कि मरी गौ की पूँछ हाथ में लेकर एक सौ गाँवों में वह व्यक्ति उच्च स्वर से चिल्ला- चिल्लाकर यह कहे कि मुझसे गौ- हत्या हो गयी। इस दोष प्रकाशन से गौ- हत्या का दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो, उससे क्षमा माँगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वह सन्तुष्ट हो सके वह करना चाहिए। यदि वह भी न हो, तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अन्तरात्मा का एक भारी बोझ तो हलका करना ही चाहिए। इस प्रकार के दोष प्रकाशन के लिये ‘शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार’ को एक विश्वसनीय मित्र समझकर पत्र द्वारा अपने दोषों को लिखकर उनके प्रायश्चित्त तथा सुधार की सलाह प्रसन्नतापूर्वक ली जा सकती है।
(८) साधना तप
गायत्री का चौबीस हजार जप नौ दिन में पूरा करना, सवालक्ष जप चालीस दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएँ, पुरश्चरण, पूजन, स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग ‘गायत्री चालीसा’ का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामन्त्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं।
(९) ब्रह्मचर्य तप
वीर्य- रक्षा, मैथुन से बचना, काम- विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम- सेवन शारीरिक काम- सेवन की ही भाँति हानिकारक है। मन को कामक्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाये रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में, सत् तत्त्व में लगाये रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर्य रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से तीन लाभ करने वाला यह तप गायत्री साधना वालों के लिये सब प्रकार उत्तम है।
(१०) चान्द्रायण तप
यह व्रत पूर्णमासी से आरम्भ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खूराक हो, उसका चौदहवाँ भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिये। कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा जैसे १- १ कला नित्य घटता है, वैसे ही १- १ चतुर्दशांश नित्य कम करते चलना चाहिये। अमावस्या और प्रतिपदा को चन्द्रमा बिलकुल दिखाई नहीं पड़ता। उन दो दिनों बिलकुल भी आहार न लेना चाहिये। फिर शुक्ल पक्ष की दूज को चन्द्रमा एक कला से निकलता है और धीरे- धीरे बढ़ता है, वैसे ही १- १ चतुर्दशांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुँच जाना चाहिये। एक मास में आहार- विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्त्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न रहना चाहिये।
अर्ध चान्द्रायण व्रत पन्द्रह दिन का होता है। उसमें भोजन का सातवाँ भाग सात दिन कम करना और सात दिन बढ़ाना होता है। बीच का एक दिन निराहार रहने का होता है। आरम्भ में अर्ध चान्द्रायण ही करना चाहिये। जब एक बार सफलता मिल जाए, तो पूर्ण चान्द्रायण के लिये कदम बढ़ाना चाहिये।
उपवास स्वास्थ्यरक्षा का बड़ा प्रभावशाली साधन है। मनुष्य से खान- पान में जो त्रुटियाँ स्वभाव या परिस्थितिवश होती रहती हैं, उनसे शरीर में दूषित या विजातीय तत्त्व की वृद्धि हो जाती है। उपवास काल में जब पेट खाली रहता है, तो जठराग्रि उन दोषों को ही पचाने लगती है। इसमें शरीर शुद्ध होता है और रक्त स्वच्छ हो जाता है। जिसकी देह में विजातीय तत्त्व नहीं होंगे और नाडिय़ों में स्वच्छ रक्त परिभ्रमण करता होगा, उसको एकाएक किसी रोग या बीमारी की शिकायत हो ही नहीं सकती ।। इसलिये स्वास्थ्यकामी पुरुष के लिये उपवास बहुत बड़े सहायक बन्धु के समान है। अन्य उपवासों से चान्द्रायण व्रत में यह विशेषता है कि इसमें भोजन का घटाना और बढ़ाना एक नियम और क्रम से होता है, जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता। अन्य लम्बे उपवासों में जिनमें भोजन को लगातार दस- पन्द्रह दिन के लिये छोड़ दिया जाता है, उपवास को खत्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और अधिकांश व्यक्ति उस समय अधिक मात्रा में अनुपयुक्त आहार कर लेने से कठिन रोगों के शिकार हो जाते हैं। यह चान्द्रायण व्रत में बिलकुल नहीं होता।
(११) मौन तप
मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, दैवी तत्त्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शान्ति का प्रादुर्भाव होता है, बहिर्मुखी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिये निश्चित करना चाहिये। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन अवधि निर्धारित करनी चाहिये। मौन काल का अधिकांश भाग एकान्त में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिन्तन में व्यतीत करना चाहिये।
(१२) अर्जन तप
विद्याध्ययन, शिल्प- शिक्षा, देशाटन, मल्ल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थी को जिस प्रकार कष्ट उठाना पड़ता है, मन मारना पड़ता है और सुविधाएँ छोडक़र कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यन्त किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। साल में थोड़ा- सा समय तो इस तपस्या में लगाना ही चाहिये, जिससे अपनी तपस्याएँ बढ़ती चलें और उनके द्वारा अधिक लोक- सेवा करना सम्भव हो सके।
सूर्य की बारह राशियाँ होती हैं, गायत्री के वह बारह तप हैं। इनमें से जो तप, जब, जिस प्रकार सम्भव हो, उसे अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिये। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के बारह महीनों में एक- एक महीने एक- एक तप करके एक वर्ष पूरा ‘तप- वर्ष’ बिताया जाए। सातवें निष्कासन तप में एक- दो बार विश्वस्त मित्रों के सामने दोष प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में एक मास तक अपनी बुराइयाँ लिखते रहना चाहिये और उन्हें अपने पथ- प्रदर्शक को दिखाना चाहिये। यह क्रम अधिक दिन तक चालू रखा जाए तो और भी उत्तम है। महात्मा गाँधी साबरमती आश्रम में अपने आश्रमवासियों की डायरी बड़े गौर से जाँचा करते थे।
अन्य तपों में प्रत्येक को प्रयोग करने के लिये अनेकों रीतियाँ हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी- थोड़ी अवधि के लिये निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिये। आरम्भ में थोड़ा और सरल तप अपनाने से पीछे दीर्घकाल तक और कठिन स्वाध्याय साधन करना भी सुलभ हो जाता है।
गायत्री साधना से पापमुक्ति
गायत्री की अनन्त कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्त्व पर विचार करते हुए हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत काँच या पारदर्शी पात्र में किसी रंग का पानी भर दिया जाए, तो उसी रंग का दीखने लगेगा, साधारणत: उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी भर दिया जाए, तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्मा स्वभावत: निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव भर जाते हैं, वह उसी प्रकार का दिखाई देने लगता है।
गीता में कहा है कि- ‘‘विद्या सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल आदि को जो समत्व बुद्धि से देखता है, वही पण्डित है।’’ इस समन्वय का रहस्य यह है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है, उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार अन्त:करण चतुष्टय रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक, विपन्न, विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए, तो आज के दुष्ट का कल ही सन्त बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास बताता है कि एक चाण्डाल कुलोत्पन्न तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया। जीवन भर वेश्यावृत्ति करने वाली गणिका आन्तरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी देवियों को प्राप्त होने वाली परमगति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पेशा करते हुए जिन्दगी गुजार देने वाले अजामिल और सदन परम भागवत भक्त कहलाए। इस प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले उच्चता को प्राप्त हुए हैं और हीन कुलोत्पन्नों को उच्च वर्ण की प्रतिष्ठा मिली है। रैदास चमार, कबीर जुलाहे, रामानुज शूद्र, षट्कोपाचार्य खटीक, तिरवल्लुवर अन्त्यज वर्ण में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊँची थी। विश्वामित्र भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे।
जहाँ पतित स्थान से ऊपर चढऩे के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, वहाँ उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम नहीं हैं। पुलस्त्य के उत्तम ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का महापण्डित रावण, मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष, अन्यायी कौरवों के समर्थक हो गये। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वसिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पाराशर ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके सन्तान उत्पन्न की। विश्वामित्र ने वेश्या पर आसक्त होकर उसे लम्बे समय तक अपने पास रखा। चन्द्रमा जैसा देवता गुरुमाता के साथ कुमार्गगामी बना। देवताओं के राजा इन्द्र को व्यभिचार के कारण शाप का भाजन होना पड़ा। ब्रह्म अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गये। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करने स्वयंवर में जा पहुँचे। सड़ी- गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलि राजा के दान में भाँजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी एक आँख गँवा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर कालिख पोती और धीरे से ‘नरो वा कुंजरो वा’ गुनगुनाकर अपने को झूठ से बचाने की प्रवञ्चना की। कहाँ तक कहें! किस- किस की कहें! इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़ों- बड़ों को स्थानच्युत हुआ पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि आन्तरिक स्थिति में हेर- फेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन सकते हैं।
शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं। पीछे संस्कार के प्रभाव से द्विज बनते हैं। असल में यह संस्कार ही है, जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बना देते हैं। गायत्री के तत्त्वज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है, जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है।
पापों का नाश आत्मतेज की प्रचण्डता से होता है। यह तेजी जितनी अधिक होती है, उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र और अधिक परिमाण में होता है। बिना धार की लोहे की छड़ से वह कार्य नहीं हो सकता, जो तीक्ष्ण तलवार से होता है। यह तेजी किस प्रकार आए? इसका उपाय तपाना और रगडऩा है। लोहे को आग में तपाकर उसमें धार बनाई जाती है और पत्थर पर रगडक़र उसे तेज किया जाता है। तब वह तलवार दुश्मन की सेना का सफाया करने योग्य होती है। हमें भी अपनी आत्मशक्ति तेज करने के लिये इसी तपाने, घिसने वाली प्रणाली को अपनाना पड़ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में ‘तप’ या ‘प्रायश्चित्त’ नाम से पुकारते हैं।
प्रायश्चित्त क्यों? कैसे?— अपराधों की निवृत्ति के लिये हर जगह दण्ड का विधान काम में लाया जाता है। बच्चे ने गड़बड़ी की कि माता की डाँट- डपट पड़ी। शिष्य ने प्रमाद किया कि गुरु ने छड़ी सँभाली। सामाजिक नियमों को भंग किया कि पंचायत ने दण्ड दिया। कानून का उल्लंघन हुआ कि जुर्माना, जेल, कालापानी या फाँसी तैयार है। ईश्वर दैविक, दैहिक, भौतिक दु:ख देकर पापों का दण्ड देता है। दण्ड विधान प्रतिशोध या प्रतिहिंसा मात्र नहीं है। ‘खून का बदला खून’ की जंगली प्रथा के कारण नहीं, दण्ड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर किया गया है। कारण यह है कि दण्ड स्वरूप जो कष्ट दिये जाते हैं, उनसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और भूल को छोडक़र उचित मार्ग पर आ जाता है। तप में ऐसी शक्ति है। तप की गर्मी से अनात्म तत्त्वों का संहार होता है।
दूसरों द्वारा दण्ड रूप में बलात् तप कराके हमारी शुद्धि की जाती है। उस प्रणाली को हम स्वयं ही अपनाएँ, अपने गुप्त- प्रकट पापों का दण्ड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छापूर्वक तप करें, तो वह दूसरों द्वारा बलात् कराये हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम है। उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा एवं न आत्मग्लानि से चित्त क्षोभित होता है, वरन् स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनन्द आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिये आत्मतेज की अग्रि चाहिए। इस अग्रि की उत्पत्ति से दुहरा लाभ होता है, एक तो हानिकारक तत्त्वों का, कषाय- कल्मषों का नाश होता है, दूसरे उनकी ऊष्मा और प्रकाश से दैवी तत्त्वों का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में पग- पग पर व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचरण- विचार आदि के विधि- विधान इसी दृष्टि से किये गये हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दुहरे लाभों को उठा सके।
‘अपने से कोई भूल, पाप या बुराइयाँ बन पड़ी हों, तो उनके अशुभ फलों के निवारण के लिये सच्चा प्रायश्चित्त तो यही है कि उन्हें फिर न करने का दृढ़ निश्चय किया जाए, पर यदि इस निश्चय के साथ- साथ थोड़ी तपश्चर्या भी की जाए, तो उसे प्रतिज्ञा का बल मिलता है और उसके पालन में दृढ़ता आती है। साथ ही यह तपश्चर्या सात्त्विकता की तीव्रगति से वृद्धि करती है, चैतन्यता उत्पन्न करती है और ऐसे उत्तमोत्तम गुण, कर्म, स्वभावों को उत्पन्न करती है, जिनसे पवित्रतामय, साधनामय, मंगलमय जीवन बिताना सुगम हो जाता है। गायत्री शक्ति के आधार पर की गयी तपश्चर्या बड़े- बड़े पापियों को भी निष्पाप बनाने, उनके पाप- पुंजों को नष्ट करने तथा भविष्य के लिये उन्हें निष्पाप रहने योग्य बना सकती है।’
क्रिया नहीं, भाव प्रधान—जो कार्य पाप दिखाई पड़ते हैं, वे सर्वदा वैसे पाप नहीं होते जैसे कि समझते हैं। कहा गया है कि कोई भी कार्य न तो पाप है न पुण्य; कर्ता की भावना के अनुसार पाप- पुण्य होते हैं। जो कार्य एक मनुष्य के लिये पाप है, वही दूसरे के लिए पापरहित है और किसी के लिये वह पुण्य भी है। हत्या करना एक कर्म है, वह तीन व्यक्तियों के लिये तीन विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिये किसी की हत्या करता है, यह हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय रक्षा के लिये प्राणदण्ड देता है, वह उसके लिये कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आततायी डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिये अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है, तो वह पुण्य है। हत्या तीनों ने ही की, पर तीनों की हत्यायें अलग- अलग परिणाम वाली हैं। तीनों हत्यारे डाकू, न्यायाधीश एवं आततायी से लड़कर उसका वध करने वाले- समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते ।।
चोरी एक बुरा कार्य है, परन्तु परिस्थितियों वश वह भी सदा बुरा नहीं रहता। स्वयं सम्पन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है, वह पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण लीजिये- भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी भी सम्पन्न व्यक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है।
तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की साधन- सामग्री चुराकर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सत्कर्म में लगा देना पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराये जा सकते।
परिस्थिति, मजबूरी, धर्मरक्षा तथा बौद्धिक स्वल्प विकास के कारणवश कई बार ऐसे कार्य होते हैं, जो स्थूल दृष्टि से देखने में निन्दनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुत: उनके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती, ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिये माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिये डाक्टर को कसाई के समान चीड़- फाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। रोगी की कुपथ्यकारक इच्छाओं को टालने के लिये उपचारक को झूठे बहाने बनाकर किसी प्रकार समझाना पड़ता है। बालकों की जिद का भी प्राय: ऐसा ही समाधान किया जाता है। हिंसक जन्तुओं, शस्त्रधारी दस्युओं पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है।
प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा है; किन्तु लोकहित, धर्मवृद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ा जैसे कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणत: बनना पड़ता है। भगवान् विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिये मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मन्थन के समय अमृतघट के बँटवारे पर जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था, तब भी विष्णु ने माया- मोहिनी का रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृन्दा का सतीत्व डिगाने के लिये भगवान् ने जालन्धर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिये वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था।
महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छलपूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने शिखण्डी की ओट से खड़े होकर भीष्म को मारा, कर्ण का रथ कीचड़ में धँस जाने पर भी उसका वध किया। घोर दुर्भिक्ष में क्षुधापीडि़त होने पर विश्वामित्र ऋषि ने चाण्डाल के घर से कुत्ते का मांस चुराकर खाया। प्रह्लाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, गोपियों का पर पुरुष श्रीकृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, परशुराम जी का अपनी माता का सिर काट देना आदि कार्य साधारणत: अधर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हें कर्ताओं ने सदुद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, इसलिये धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से यह कार्य पातक नहीं गिन गये।
परिस्थिति, मजबूरी, धर्मरक्षा तथा बौद्धिक स्वल्प विकास के कारणवश कई बार ऐसे कार्य होते हैं, जो स्थूल दृष्टि से देखने में निन्दनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुत: उनके पीछे पाप भावना छिपी हुई नहीं होती, ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। बालक का फोड़ा चिरवाने के लिये माता को उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और बालक को कष्ट में डालना पड़ता है। रोगी की प्राण रक्षा के लिये डाक्टर को कसाई के समान चीड़- फाड़ करने का कार्य करना पड़ता है। रोगी की कुपथ्यकारक इच्छाओं को टालने के लिये उपचारक को झूठे बहाने बनाकर किसी प्रकार समझाना पड़ता है। बालकों की जिद का भी प्राय: ऐसा ही समाधान किया जाता है। हिंसक जन्तुओं, शस्त्रधारी दस्युओं पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है।
प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा है; किन्तु लोकहित, धर्मवृद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ा जैसे कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणत: बनना पड़ता है। भगवान् विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिये मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मन्थन के समय अमृतघट के बँटवारे पर जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था, तब भी विष्णु ने माया- मोहिनी का रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया। सती वृन्दा का सतीत्व डिगाने के लिये भगवान् ने जालन्धर का रूप बनाया था। राजा बलि को छलने के लिये वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था।
महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छलपूर्वक समर्थन किया। अर्जुन ने शिखण्डी की ओट से खड़े होकर भीष्म को मारा, कर्ण का रथ कीचड़ में धँस जाने पर भी उसका वध किया। घोर दुर्भिक्ष में क्षुधापीडि़त होने पर विश्वामित्र ऋषि ने चाण्डाल के घर से कुत्ते का मांस चुराकर खाया। प्रह्लाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, गोपियों का पर पुरुष श्रीकृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, परशुराम जी का अपनी माता का सिर काट देना आदि कार्य साधारणत: अधर्म प्रतीत होते हैं, पर उन्हें कर्ताओं ने सदुद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, इसलिये धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से यह कार्य पातक नहीं गिन गये।
शिवाजी ने अफजल खाँ का वध कूटनीतिक चातुर्य से किया था। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रान्तिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को
अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का समावेश हुआ था जो मोटे तौर से अधर्म कहे जाते हैं; परन्तु उनकी आत्मा पवित्र थी, असंख्य दीन- दु:खी प्रजा की करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासन को उलटने के लिये ही उन्होंने ऐसा किया था। कानून उनको भले ही अपराधी बताए, पर वस्तुत: वे पापी कदापि नहीं कहे जा सकते।
अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिये भगवान् को युग- युग में अवतार लेकर अगणित हत्यायें करनी पड़ती हैं और रक्त की धार बहानी पड़ती है। इसमें पाप नहीं होता। सदुद्देश्य के लिये किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है। इस प्रकार मजबूर किये गये, सताये गये, बुभुक्षित, सन्त्रस्त, दु:खी, उत्तेजित, आपत्तिग्रस्तों, अज्ञानी बालक, रोगी अथवा पागल कोई अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो वह क्षम्य माने जाते हैं; कारण यह है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक विचार करने में समर्थ नहीं होता।
पापियों की सूची में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं, जिन्हें उपर्युक्त किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े, पीछे वे उनके स्वभाव में आ गये। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गये। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियाँ, सुविधायें उन्हें मिलतीं, ऊँचा उठाने वाले और सन्तोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चय ही वे अच्छे बने होते।
कानून और लोकमत चाहे किसी को कितना ही दोषी ठहरा सकता है, स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यन्त बुरा हो सकता है, पर वास्तविक पापियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। जो परिस्थितियों के वश बुरे बन गये हैं, उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण तत्त्वत: पवित्र है। बुराई उसके ऊपर छाया मैल है। मैल को साफ करना न तो असम्भव है और न कष्टसाध्य, वरन् यह कार्य आसानी से हो सकता है।
कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किये हैं, इतनी बुराइयाँ की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, अब हम सुधर नहीं सकते, हमें न जाने कब तक नरक में सडऩा पड़ेगा! हमारा उद्धार और कल्याण अब कैसे हो सकता है? ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिये कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली- कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुएँ भी उसी में रह जाते हैं। पाप- वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित्त करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिये भाग्य बन चुके हैं, उन्हें तो किसी न किसी रूप से भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन या आजकल के ऐसे कर्म हैं, जो अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, उनका संचित समूह नष्ट हो जाता है। जो इस जन्म के लिए दु:खदायी भोग हैं, वे भी अपेक्षाकृत बहुत हलके हो जाते हैं और चिह्न- पूजा मात्र थोड़ा कष्ट दिखाकर सहज ही शान्त हो जाते हैं।
कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत- सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिये केवल दु:ख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है, वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व एक सप्ताह आत्मकल्याण के लिये मिला था। उसने इस थोड़े समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को जन्म भर की व्यभिचारिणी आदतों से छुटकारा न मिलते देखकर अन्त में आँखे फोड़ लेनी पड़ी थीं। तुलसीदास का कामातुर होकर रातो- रात ससुराल पहुँचना और परनाले में लटका हुआ साँप पकडक़र स्त्री के पास जा पहुँचना प्रसिद्ध है। इस प्रकार के असंख्यों व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरे कार्यों में व्यतीत करने के उपरान्त सत्पथगामी हुए और थोड़े से ही समय में योगियों और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति के अधिकारी हुए हैं।
यह एक रहस्यमय तथ्य है कि मन्दबुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबियत के सीधे कहलाने वालों की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं, जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदमाश रहे हैं। कारण यह है कि मन्द चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत न्यून होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहें, तो भी मन्द शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यन्त मन्द गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अन्दर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे, उधर ही ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में झण्डा बुलन्द रखा है, वे निश्चय ही शक्ति सम्पन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमार्गगामी रही है। यदि वह शक्ति सत्पथ पर लग जाए तो उस दिशा में भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा एक वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी उतना एक दिन में ही ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है; इस मञ्जिल पर वे ही लोग शीघ्र पहुँच सकते हैं, जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायुओं में बल और मन में अदम्य साहस तथा उत्साह है।
जो लोग पिछले जीवन में कुमार्गगामी रहे हैं, बड़ी ऊटपटाँग, गड़बड़ करते रहे हैं, वे भूले हुए पथभ्रष्ट तो अवश्य हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, जागरूकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया है। यह बढ़ोत्तरी एक अच्छी पूँजी है। पथभ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े, वे पश्चात्ताप और दु:ख के हेतु अवश्य हैं। सन्तोष की बात इतनी है कि उस कँटीले- पथरीले, लहू- लुहान करने वाले, ऊबड़- खाबड़, दु:खदायी मार्ग में भटकते हुए भी मञ्जिल की दिशा में ही यात्रा की है। यदि अब सँभल जाया जाए और सीधे राजमार्ग से सतोगुणी आधार से आगे बढ़ा जाए तो पिछला ऊल- जलूल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा।
पाप और दोषों का प्रधान कारण प्राय: दूषित मानसिक भावनायें ही हुआ करती हैं। इन गर्हित भावनाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे वह अकरणीय कार्य करता रहता है। इस कारण होने वाले पापों से छुटकारा पाने का उपाय यही है कि मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे विचारों का शमन और निराकरण करे। जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए, तो उसमें हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर सुमार्गगामी बन जायेगा। इसके लिये स्वाध्याय, सत्संग आदि को प्रभावशाली साधन बतलाया है। गायत्री मन्त्र सद्बुद्धि का प्रेरणादायक होने से स्वाध्याय का एक बड़ा अङ्ग माना जा सकता है। जब उससे मन श्रेष्ठ विचारों की तरफ जाता है, तो असद्बुद्धि का स्वयं ही अन्त होने लग जाता है। किसी भावना के लगातार चिन्तन में बड़ी शक्ति होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि और शुभ विचारों का चिन्तन करते रहेंगे, तो पापयुक्त भावनाओं का क्षीण होते जाना स्वाभाविक ही है।
पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं; कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गये हैं, वे थोड़ा दु:ख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। उसके लिये चिन्ता एवं निराशा की कोई बात नहीं, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। यह परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति करते हैं और स्वल्पकाल में ही सच्चे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण वे सख्त बदमाश थे, वे ही विशेषतायें उन्हें सफल सन्त बना देती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे, बदमाश और दुराचारी स्त्री- पुरुष भी स्वल्पकाल में सन्मार्गगामी और पापरहित हो सकते हैं।
कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत- सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिये केवल दु:ख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है, वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व एक सप्ताह आत्मकल्याण के लिये मिला था। उसने इस थोड़े समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को जन्म भर की व्यभिचारिणी आदतों से छुटकारा न मिलते देखकर अन्त में आँखे फोड़ लेनी पड़ी थीं। तुलसीदास का कामातुर होकर रातो- रात ससुराल पहुँचना और परनाले में लटका हुआ साँप पकडक़र स्त्री के पास जा पहुँचना प्रसिद्ध है। इस प्रकार के असंख्यों व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरे कार्यों में व्यतीत करने के उपरान्त सत्पथगामी हुए और थोड़े से ही समय में योगियों और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति के अधिकारी हुए हैं।
यह एक रहस्यमय तथ्य है कि मन्दबुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबियत के सीधे कहलाने वालों की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं, जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदमाश रहे हैं। कारण यह है कि मन्द चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत न्यून होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहें, तो भी मन्द शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यन्त मन्द गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अन्दर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे, उधर ही ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में झण्डा बुलन्द रखा है, वे निश्चय ही शक्ति सम्पन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमार्गगामी रही है। यदि वह शक्ति सत्पथ पर लग जाए तो उस दिशा में भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा एक वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी उतना एक दिन में ही ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है; इस मञ्जिल पर वे ही लोग शीघ्र पहुँच सकते हैं, जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायुओं में बल और मन में अदम्य साहस तथा उत्साह है।
जो लोग पिछले जीवन में कुमार्गगामी रहे हैं, बड़ी ऊटपटाँग, गड़बड़ करते रहे हैं, वे भूले हुए पथभ्रष्ट तो अवश्य हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, जागरूकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया है। यह बढ़ोत्तरी एक अच्छी पूँजी है। पथभ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े, वे पश्चात्ताप और दु:ख के हेतु अवश्य हैं। सन्तोष की बात इतनी है कि उस कँटीले- पथरीले, लहू- लुहान करने वाले, ऊबड़- खाबड़, दु:खदायी मार्ग में भटकते हुए भी मञ्जिल की दिशा में ही यात्रा की है। यदि अब सँभल जाया जाए और सीधे राजमार्ग से सतोगुणी आधार से आगे बढ़ा जाए तो पिछला ऊल- जलूल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा।
पाप और दोषों का प्रधान कारण प्राय: दूषित मानसिक भावनायें ही हुआ करती हैं। इन गर्हित भावनाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे वह अकरणीय कार्य करता रहता है। इस कारण होने वाले पापों से छुटकारा पाने का उपाय यही है कि मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे विचारों का शमन और निराकरण करे। जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए, तो उसमें हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर सुमार्गगामी बन जायेगा। इसके लिये स्वाध्याय, सत्संग आदि को प्रभावशाली साधन बतलाया है। गायत्री मन्त्र सद्बुद्धि का प्रेरणादायक होने से स्वाध्याय का एक बड़ा अङ्ग माना जा सकता है। जब उससे मन श्रेष्ठ विचारों की तरफ जाता है, तो असद्बुद्धि का स्वयं ही अन्त होने लग जाता है। किसी भावना के लगातार चिन्तन में बड़ी शक्ति होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि और शुभ विचारों का चिन्तन करते रहेंगे, तो पापयुक्त भावनाओं का क्षीण होते जाना स्वाभाविक ही है।
पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं; कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गये हैं, वे थोड़ा दु:ख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। उसके लिये चिन्ता एवं निराशा की कोई बात नहीं, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। यह परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति करते हैं और स्वल्पकाल में ही सच्चे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण वे सख्त बदमाश थे, वे ही विशेषतायें उन्हें सफल सन्त बना देती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे, बदमाश और दुराचारी स्त्री- पुरुष भी स्वल्पकाल में सन्मार्गगामी और पापरहित हो सकते हैं।
Versions
-

ENGLISHSuper Science of GayatriScan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानScan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 1Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 2Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 3Scan Book Version
-
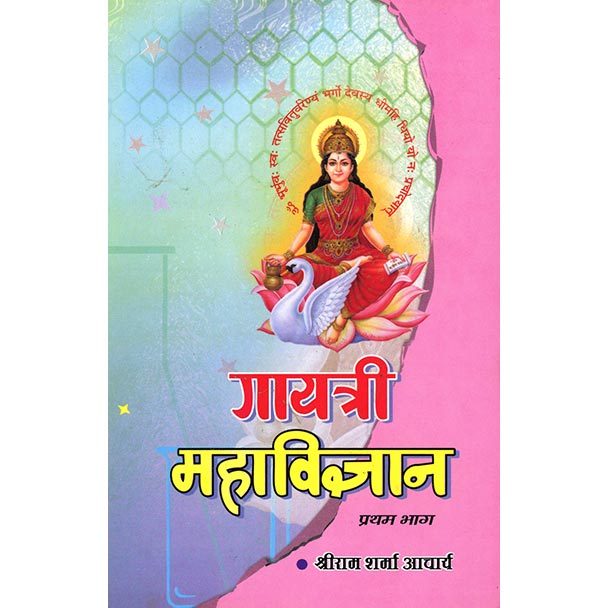
MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग १Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग २Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग ३Scan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानText Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग)Text Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान भाग 2Text Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री महाविज्ञान भाग १
- वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति
- ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव
- गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है
- गायत्री साधना से शक्तिकोशों का उद्भव
- शरीर में गायत्री मंत्र के अक्षर
- गायत्री और ब्रह्म की एकता
- महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान
- त्रिविध दु:खों का निवारण
- गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना
- गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता
- गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण
- जीवन का कायाकल्प
- नारियों को वेद एवं गायत्री का अधिकार
- देवियों की गायत्री साधना
- गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य
- गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत (जनेऊ)
- साधकों के लिये उपवीत आवश्यक है
- गायत्री साधना का उद्देश्य
- निष्काम साधना का तत्त्व ज्ञान
- गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध
- साधना- एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- आत्मशक्ति का अकूत भण्डार :: अनुष्ठान
- सदैव शुभ गायत्री यज्ञ
- महिलाओं के लिये विशेष साधनाएँ
- एक वर्ष की उद्यापन साधना
- गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि
- गायत्री का अर्थ चिन्तन
- साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते
- साधना की सफलता के लक्षण
- सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिये
- गायत्री द्वारा कुण्डलिनी जागरण
- यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बाँटिये
- गायत्री महाविज्ञान भाग ३ भूमिका
- गायत्री के पाँच मुख
- अनन्त आनन्द की साधना
- गायत्री मञ्जरी
- अन्नमय कोश और उसकी साधना
- उपवास - अन्नमय कोश की साधना
- आसन - अन्नमय कोश की साधना
- तत्त्व शुद्धि - अन्नमय कोश की साधना
- तपश्चर्या - अन्नमय कोश की साधना
- मनोमय कोश की साधना
- ध्यान - मनोमय कोश की साधना
- त्राटक - मनोमय कोश की साधना
- जप - मनोमय कोश की साधना
- तन्मात्रा साधना - मनोमय कोश की साधना
- विज्ञानमय कोश की साधना
- सोऽहं साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मानुभूति योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मचिन्तन की साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- स्वर योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- वायु साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- ग्रन्थि-भेद - विज्ञानमय कोश की साधना
- आनन्दमय कोश की साधना
- नाद साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- बिन्दु साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- कला साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- तुरीयावस्था - आनन्दमय कोश की साधना
- पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य
- गायत्री-साधना निष्फल नहीं जाती
- पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य
- गायत्री का तन्त्रोक्त वाम-मार्ग
- गायत्री की गुरु दीक्षा
- आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- मन्त्र दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- अग्नि दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्म दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- कल्याण मन्दिर का प्रवेश द्वार - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्मदीक्षा की दक्षिणा आत्मदान - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- वर्तमानकालीन कठिनाइयाँ - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ

