गायत्री महाविज्ञान 
गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध
Read Scan Version
यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। हमारे धर्म में जितनी महानता यज्ञ को दी गयी है, उतनी और किसी को नहीं दी गयी है। हमारा कोई भी शुभ- अशुभ, धर्मकृत्य यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं होता। जन्म से लेकर अन्त्येष्टि तक १६ संस्कार होते हैं, इनमें अग्रिहोत्र आवश्यक है। जब बालक का जन्म होता है तो उसकी रक्षार्थ सूतक निवृत्ति तक घर में अखण्ड अग्रि स्थापित रखी जाती है। नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों में भी हवन अवश्य होता है। अन्त मं जब शरीर छूटता है तो उसे अग्रि को ही सौंपते हैं। अब लोग मृत्यु के समय चिता जलाकर यों ही लाश को भस्म कर देते हैं, पर शास्त्रों में देखा जाए, तो वह भी एक संस्कार है। इसमें वेदमन्त्रों से विधिपूर्वक आहुतियाँ चढ़ाई जाती हैं और शरीर यज्ञ भगवान् को समर्पित किया जाता है।
प्रत्येक कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, उत्सव, उद्यापन में हवन को आवश्यक माना जाता है। अब लोग इसका महत्त्व और इसका विधान भूल गये हैं और केवल चिह्न- पूजा करके काम चला लेते हैं। घरों में स्त्रियाँ किसी रूप में यज्ञ की पूजा करती हैं। वे त्योहारों या पर्वों पर ‘अग्रि को जिमाने’ या ‘अगियारी’ करने का कृत्य किसी न किसी रूप में करती रहती हैं। थोड़ी- सी अग्रि लेकर उस पर घी डालकर प्रज्वलित करना और उस पर पकवान के छोटे- छोटे ग्रास चढ़ाना और फिर जल से अग्रि की परिक्रमा कर देना- यह विधान हम घर- घर में प्रत्येक पर्व एवं त्योहारों पर होते देख सकते हैं। पितरों का श्राद्ध जिस दिन होगा, उस दिन ब्राह्मण भोजन से पूर्व इस प्रकार अग्रि को भोजन अवश्य कराया जायेगा, क्योंकि यह स्थिर मान्यता है कि अग्रि के मुख में दी हुई आहुति देवताओं और पितरों तक अवश्य पहुँचती है।
विशेष अवसर पर तो हवन करना ही पड़ता है। नित्य की चूल्हा, चक्की, बुहारी आदि से होने वाली जीव हिंसा एवं पातकों के निवारणार्थ नित्य पंच यज्ञ करने का विधान है। उन पाँचों में बलिवैश्व भी है। बलिवैश्व अग्रि में आहुति देने से होता है। इस प्रकार तो शास्त्रों की आज्ञानुसार नित्य हवन करना भी हमारे लिये आवश्यक है। होली तो यज्ञ का त्योहार है। आजकल लोग लकड़ी उपले जलाकर होली मनाते हैं। शास्त्रों में देखा जाये तो यह भी यज्ञ है। लोग यज्ञ की आवश्यकता और विधि को भूल गये, पर केवल ईन्धन जलाकर उस प्राचीन परम्परा की किसी प्रकार पूर्ति कर देते हैं। इसी प्रकार श्रावणी, दशहरा, दीपावली के त्योहारों पर किसी न किसी रूप में हवन अवश्य होता है। नवरात्र में स्त्रियाँ देवी की पूजा करती हैं, तो अग्रि के मुख में देवी के निमित्त घी, लौंग, जायफल आदि अवश्य चढ़ाती हैं। सत्यनारायण व्रत कथा, रामायण- पारायण, गीता- पाठ, भागवत- सप्ताह आदि कोई भी शुभ कर्म क्यों न हो, हवन इसमें अवश्य रहेगा।
साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरश्चरण, जप, साधन किये जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हों, चाहे तान्त्रिक, हवन किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरश्चरण में जप से दसवाँ भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश दशवाँ भाग आहुति न दी जा सके, तो शतांश (सौवाँ भाग) आवश्यक ही है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का जन्म होता है, जिसे ‘द्विजत्व’ कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है- दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता- पिता की सेवा- पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म- कर्त्तव्य है।
धर्मग्रन्थों में पग- पग पर यज्ञ की महिमा का गान है। वेद में यज्ञ विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। भगवान् यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। कहा गया है—
यो यज्ञै: यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंज्ञित:।
तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम्॥
‘‘जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय हैं, यज्ञ रूप हैं, उन यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान् को नमस्कार है।’’
यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोडऩे वालों की शास्त्रों में बहुत निन्दा की गयी है—
कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति। पोषाय रक्षसां भागोसि॥ यजु. २.२३
‘‘सुख- शान्ति चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नहीं करता। जो यज्ञ को छोड़ता है, उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी छोड़ देते हैं। सबकी उन्नति के लिये आहुतियाँ यज्ञ में छोड़ी जाती हैं; जो आहुति नहीं छोड़ता, वह राक्षस हो जाता है।’’
यज्ञेन पापै: बहुभिर्विमुक्त: प्राप्रोति लोकान् परमस्य विष्णो:। -हारीत
‘‘यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक की भी प्राप्ति होती है।’’
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धनार्थी लभते धनम्।
भार्यार्थी शोभनां भार्यां कुमारी च शुभं पतिम्॥
भ्रष्ट राज्यस्तथा राज्यं श्रीकाम: श्रियमाप्रुयात्।
यं यं प्रार्थयते कामं स वै भवति पुष्कल:॥
निष्काम: कुरुते यस्तु स परंब्रह्म गच्छति। —मत्स्यपुराण ९३/११७- ११८
यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, विवाहार्थी को सुन्दर भार्या, कुमारी को सुन्दर पति, श्री कामना वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है और निष्काम भाव से यज्ञानुष्ठन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है।
न तस्य ग्रहपीडा स्यान्नच बन्धु- धनक्षय:।
ग्रह यज्ञ व्रतं गेहे लिखितं यत्र तिष्ठन्ति
न तत्र पीडा पापानां न रोगो न च बन्धनम्।
अशेष- यज्ञ -कोटि होम पद्धति
यज्ञ करने वाले को ग्रह पीड़ा, बन्धु नाश, धन क्षय, पाप, रोग, बन्धन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यज्ञ का फल अनन्त है।
देवा: सन्तोषिता यज्ञैर्लोकान् सम्बन्धयन्त्युत।
उभयोर्लोकयोर्देव भूतिर्यज्ञ: प्रदृश्यते॥
तस्माद्यद् याति देवत्वं पूर्वजै: सह मोदते।
नास्ति यज्ञ समं दानं नास्ति यज्ञ समो विधि:॥
सर्वधर्म समुद्देश्यो देवयज्ञे समाहित:॥
‘‘यज्ञों से सन्तुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ द्वारा लोक- परलोक का सुख प्राप्त हो सकता है। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि- विधान नहीं; यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है।’’
असुराश्च सुराश्चैव पुण्यहेतोर्मख- क्रियाम्।
प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्यज्ञा:परायणा:।
यज्ञैरेव महात्मानो बभूवुरधिका: सुरा:॥ महाभारत आश्व० ३.६,७
‘‘असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिये प्रयत्न करते हैं। सत्पुरुषों को सदा यज्ञपरायण होना चाहिये। यज्ञों से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने हैं।’’
यदिक्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।
तमाहरामि निर्ऋते रुपस्थादस्पार्शमेनं शत- शारदाय॥ -अथर्व० ३/११/२
‘‘यदि रोगी अपनी जीवनी शक्ति को खो भी चुका हो, निराशाजनक स्थिति को पहुँच गया हो, यदि मरणकाल भी समीप आ पहुँचा हो, तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है और सौ वर्ष जीवित रहने के लिये पुन: बलवान् बना देता है।’’
यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्टयुत्सर्गेण वै प्रजा:।
आप्यायन्ते तु धर्मज्ञ! यज्ञा: कल्याण- हेतव:॥ -विष्णु पुराण
‘‘यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है। यज्ञ द्वारा वर्षा होती है। वर्षा से अन्न और प्रजापालन होता है। हे धर्मज्ञ! यज्ञ ही कल्याण का हेतु है।’’
प्रयुक्तया यया चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जित:।
तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्॥ -चरक चि० खण्ड ८/११२
‘‘तपेदिक सरीखे रोगों को प्राचीनकाल में यज्ञ के प्रयोगों से नष्ट किया जाता था। रोगमुक्ति की इच्छा रखने वालों को चाहिये कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय लें।’’
अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्रिरहं हुतम्॥ -गीता ९/१६
‘‘मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ और मन्त्र, घृत, अग्रि तथा हवन भी मैं ही हूँ।’’
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य: कुरुसत्तम। -गीता ४/३१
‘‘हे अर्जुन! यज्ञरहित मनुष्य को इस लोक में भी सुख नहीं मिल सकता, फिर परलोक का सुख तो होगा ही कैसे?’’
नास्ति अयज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते शुभम्।
अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यतिच्छिन्नपर्णवत्॥ -शंख स्मृति
‘‘यज्ञ न करने वाला मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखों से वंचित हो जाता है। यज्ञ न करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती और वह पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट हो जाता है।’’
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्व पुरोवाच प्रजापति:।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:।
परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ॥
इष्टन्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:। -गीता ३/१०- ११
‘‘ब्रह्मजी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी। यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं की पुष्टि करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने- अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किये हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख- शान्ति की वस्तुयें प्रदान करेंगे।’’
असंख्यों शास्त्र वचनों में से कुछ प्रमाण ऊपर दिये गये हैं। इनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्वकाल में आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े- बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वारा यज्ञ किये जाते थे, राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे, साधारण गृहस्थ अपनी- अपनी सामर्थ्यों के अनुसार समय- समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर लोग सदैव यज्ञों को विध्वंस करने का प्रयत्न इसलिये किया करते थे कि उनके शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष न होने पाये। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का विध्वंस भी कराया गया है। रामायण में राक्षसों के ऐसे यज्ञ का वर्णन है, जिसे हनुमान् जी ने नष्ट किया था। यदि वह सफल हो जाता, तो राक्षस अजेय हो जाते।
राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके चार पुत्र पाये थे। राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इन्द्रासन के अधिकारी हुए थे। राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा सन्तान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। इन्द्र ने स्वयं भी यज्ञों द्वारा ही स्वर्ग पाया था। भगवान् राम अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया था। श्रीकृष्ण जी की प्रेरणा से पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें श्रीकृष्ण जी ने आगन्तुकों के स्वागत- सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। पापों के प्रायश्चित्त स्वरूप, अनिष्टों और प्रारब्धजन्य दुर्भाग्यों की शान्ति के निमित्त, किसी अभाव की पूर्ति के लिये, कोई सहयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से, रोग निवारणार्थ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, धन- धान्य की अधिक उपज के लिये अमृतमयी वर्षा के निमित्त, वायु मण्डल में से अस्वास्थ्यकर तत्त्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन- यज्ञ किये जाते थे और उनका परिणाम भी वैसा ही होता था।
यज्ञ एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की समिधायें काम में ली जाती हैं, उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिये किस प्रकार की हव्य वस्तुयें होमी जाती हैं, उनका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमण्डल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेदमन्त्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं, उन पर तथा निकटवर्ती वायुमण्डल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अन्तराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं, उन्हें देवता कहते हैं। उन देवताओं को अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा में प्रयोग करना, उनसे सम्बन्ध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न करना है। यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है।
संसार में कभी भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूपान्तर होता रहता है। जो वस्तुएँ हवन में होमी जाती हैं, वे तथा वेदमन्त्रों की शक्ति के साथ जो सद्भावनाएँ यज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, वे दोनों मिलकर आकाश में छा जाती हैं। उनका प्रवाह समस्त संसार के लिए कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार यह संसार की सेवा का, विश्व में सुख- शान्ति उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य परमार्थ है। यज्ञ से याज्ञिक की आत्मशुद्धि होती है, उनके पाप- ताप नष्ट होते हैं तथा शान्ति एवं सद्गति उपलब्ध होती है। सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले मनुष्यों का लोक- परलोक सुधरता है। यदि उनका पुण्य पर्याप्त हुआ, तब तो उन्हें स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा यदि दूसरा जन्म भी लेना पड़ा, तो सुखी, श्रीमान्, साधन- सम्पन्न उच्च परिवार में जन्म होता है, ताकि आगे के लिए वह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुआ लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।
यज्ञ का अर्थ- दान, एकता, उपासना से है। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन, शक्तिशाली मन्त्रों का विधिवत् उच्चारण, विधिपूर्वक बनाये हुए कुण्ड, शास्त्रोक्त समिधाएँ तथा सामग्रियाँ जब ठीक विधानपूर्वक हवन की जाती हैं, तो उनका दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मण्डल में फैल जाता है। उसके प्रभाव के फलस्वरूप प्रजा के अन्त:करण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों एवं सद्विचारों का स्वयमेव आविर्भाव होने लगता है। पत्तों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के स्थान पर जो सन्तान पैदा होती है, वह स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है। पूर्वकाल में पुत्र प्राप्ति के लिए ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हों, सो बात नहीं; जिनको बराबर सन्तानें प्राप्त होती थीं, वे भी सद्गुणी एवं प्रतिभावान सन्तान प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे। गर्भाधान, सीमान्त, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि संस्कार बालक के जन्म लेते- लेते अबोध अवस्था में ही हो जाते थे। इनमें से प्रत्येक में हवन होता था, ताकि बालक के मन पर दिव्य प्रभाव पड़ें और वह बड़ा होने पर पुरुष सिंह एवं महापुरुष बने। प्राचीनकाल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों और बुरी आदतों से ग्रसित बालकों से ही हमारे घर भरे हुए हैं।
यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत् तरंगें फैलती हैं, वे लोगों के मनों से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती हैं। फलस्वरूप उससे अनेकों समस्याएँ हल होती हैं; अनेकों उलझनें, गुत्थियाँ, पेचीदगियाँ, चिन्ताएँ, भय, आशंकाएँ तथा बुरी सम्भावनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं। राजा, धनी, सम्पन्न लोग, ऋषि- मुनि बड़े- बड़े यज्ञ करते थे, जिससे दूर- दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयाँ तथा उलझनें सुलझती थीं।
बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है। उसमें जो कुछ खिलाया जाता है, वह सच्चे अर्थों में ब्रह्मभोज है। ब्रह्म अर्थात् परमात्मा, भोज अर्थात् भोजन; परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोडऩा ही है। भगवान् हम सबको खिलाता है। हमारा भी कर्त्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी न करें। जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वे कई व्यक्ति थोड़ा- थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ साधन सुयोग न हों, वहाँ यदा- कदा छोटे- छोटे हवन किये जा सकते हैं अथवा जहाँ नियमित यज्ञ होते हैं, वहाँ अपनी ओर से कुछ आहुतियों का हवन कराया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति यज्ञ कर रहे हों, तो उसमें समय, सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न भी यज्ञ में भागीदार होना ही है।
हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यज्ञ में जो कुछ धन, सामग्री, श्रम लगाया जाता है, वह कभी निरर्थक नहीं जाता। एक प्रकार से वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है और उचित अवसर पर सन्तोषजनक ब्याज समेत वापस मिल जाता है। विधिपूर्वक शास्त्रीय पद्धति और विशिष्ट उपचारों तथा विधानों के साथ किये गये हवन तो और भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। वे एक प्रकार से दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। पूर्वकाल में यज्ञ के द्वारा मनोवाँछित वर्षा होती थी, योद्धा लोग युद्ध में विजयश्री प्राप्त करते थे और योगी आत्मसाक्षात्कार करते थे। यज्ञ को वेदों में ‘कामधुक्’ कहा है, जिसका आशय यही है कि वह मनुष्य के सभी अभावों और बाधाओं को दूर करने वाला है।
नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। उसमें कुछ इतना भारी खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा न सके। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते, वे सप्ताह में एक बार रविवार या अमावस्या, पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। विधि- विधान भी इन साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है। ‘गायत्री यज्ञ विधान’ पुस्तक में उसकी सरल विधियाँ बताई जा चुकी हैं। उनके आधार पर बिना पण्डित- पुरोहित की सहायता के कोई भी द्विज आसानी से वह करा सकता है। जहाँ कुछ भी विधान न मालूम हो, वहाँ केवल शुद्ध घृत की आहुतियाँ गायत्री मन्त्र के अन्त में ‘स्वाहा’ शब्द लगाते हुए दी जा सकती हैं। किसी न किसी रूप में यज्ञ परम्परा को जारी रखा जाए, तो वह भारतीय संस्कृति की एक बड़ी भारी सेवा है।
साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है। उससे घर की वायु शुद्धि, रोग- निवृत्ति एवं अनिष्टों से आत्मरक्षा होती है। फिर विशेष आयोजन के साथ विधि- विधानपूर्वक किये गये यज्ञ तो असाधारण फल उत्पन्न करते हैं। यह एक विद्या है। पाँचों तत्त्वों के होम में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है जिससे एक प्रचण्ड शक्ति को ‘‘द्वि मूर्धा, द्वि नासिका, सप्तहस्त, द्वि मुख, सप्तजिह्व, उत्तर मुख, कोटि द्वादश मूर्धा, द्वि पंचाशत्कला युतम्’’ आदि विशेषण युक्त कहा गया है। इस रहस्यपूर्ण संकेत में यह बताया गया है कि यज्ञाग्रि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। ये क्षेत्र सफल बनाये जा सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिका हैं, उन पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सातों प्रकार की सम्पदायें यज्ञाग्रि के हाथ में हैं, वाममार्ग और दक्षिणमार्ग ये दो मुख हैं, सातों लोक जिह्वयें हैं। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएँ हैं, वे यज्ञाग्रि के मुख में मौजूद हैं। उत्तर ध्रुव का चुम्बकत्व केन्द्र अग्रि मुख है। ५२ कलायें यज्ञ की ऐसी हैं, जिनमें से कुछ को ही प्राप्त करके रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि यह सभी कलायें उपलब्ध हो जाएँ, तो मनुष्य साक्षात् अग्रि स्वरूप हो सकता है और विश्व के सभी पदार्थ उसके करतलगत हो सकते हैं। यज्ञ की महिमा अनन्त है और उसका आयोजन भी फलदायक होता है। गायत्री उपासकों के लिए तो यज्ञ पिता तुल्य पूजनीय है। यज्ञ भगवान् की पूजा होती रहे, यह प्रयत्न करना आवश्यक है।
इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं
मन्त्रों की साधना की एक विशेष विधि- व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्मकाण्ड के अनुसार मन्त्रों का अनुष्ठान साधन, पुरश्चरण करना होता है। आमतौर से अविधिपूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उससे अनिष्ट की सम्भावना रहती है।
ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मन्त्र या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तान्त्रिक अनुष्ठान किया, पर साधना की नीति- रीति में कोई भूल हो गयी या किसी प्रकार अनुष्ठान खण्डित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पडऩा पड़ा। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी हैं। वृत्र और इन्द्र की कथा इसी प्रकार की है। वेदमन्त्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था।
प्रत्येक कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, उत्सव, उद्यापन में हवन को आवश्यक माना जाता है। अब लोग इसका महत्त्व और इसका विधान भूल गये हैं और केवल चिह्न- पूजा करके काम चला लेते हैं। घरों में स्त्रियाँ किसी रूप में यज्ञ की पूजा करती हैं। वे त्योहारों या पर्वों पर ‘अग्रि को जिमाने’ या ‘अगियारी’ करने का कृत्य किसी न किसी रूप में करती रहती हैं। थोड़ी- सी अग्रि लेकर उस पर घी डालकर प्रज्वलित करना और उस पर पकवान के छोटे- छोटे ग्रास चढ़ाना और फिर जल से अग्रि की परिक्रमा कर देना- यह विधान हम घर- घर में प्रत्येक पर्व एवं त्योहारों पर होते देख सकते हैं। पितरों का श्राद्ध जिस दिन होगा, उस दिन ब्राह्मण भोजन से पूर्व इस प्रकार अग्रि को भोजन अवश्य कराया जायेगा, क्योंकि यह स्थिर मान्यता है कि अग्रि के मुख में दी हुई आहुति देवताओं और पितरों तक अवश्य पहुँचती है।
विशेष अवसर पर तो हवन करना ही पड़ता है। नित्य की चूल्हा, चक्की, बुहारी आदि से होने वाली जीव हिंसा एवं पातकों के निवारणार्थ नित्य पंच यज्ञ करने का विधान है। उन पाँचों में बलिवैश्व भी है। बलिवैश्व अग्रि में आहुति देने से होता है। इस प्रकार तो शास्त्रों की आज्ञानुसार नित्य हवन करना भी हमारे लिये आवश्यक है। होली तो यज्ञ का त्योहार है। आजकल लोग लकड़ी उपले जलाकर होली मनाते हैं। शास्त्रों में देखा जाये तो यह भी यज्ञ है। लोग यज्ञ की आवश्यकता और विधि को भूल गये, पर केवल ईन्धन जलाकर उस प्राचीन परम्परा की किसी प्रकार पूर्ति कर देते हैं। इसी प्रकार श्रावणी, दशहरा, दीपावली के त्योहारों पर किसी न किसी रूप में हवन अवश्य होता है। नवरात्र में स्त्रियाँ देवी की पूजा करती हैं, तो अग्रि के मुख में देवी के निमित्त घी, लौंग, जायफल आदि अवश्य चढ़ाती हैं। सत्यनारायण व्रत कथा, रामायण- पारायण, गीता- पाठ, भागवत- सप्ताह आदि कोई भी शुभ कर्म क्यों न हो, हवन इसमें अवश्य रहेगा।
साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरश्चरण, जप, साधन किये जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हों, चाहे तान्त्रिक, हवन किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरश्चरण में जप से दसवाँ भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश दशवाँ भाग आहुति न दी जा सके, तो शतांश (सौवाँ भाग) आवश्यक ही है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का जन्म होता है, जिसे ‘द्विजत्व’ कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है- दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता- पिता की सेवा- पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म- कर्त्तव्य है।
धर्मग्रन्थों में पग- पग पर यज्ञ की महिमा का गान है। वेद में यज्ञ विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। भगवान् यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। कहा गया है—
यो यज्ञै: यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंज्ञित:।
तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम्॥
‘‘जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय हैं, यज्ञ रूप हैं, उन यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान् को नमस्कार है।’’
यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोडऩे वालों की शास्त्रों में बहुत निन्दा की गयी है—
कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति। पोषाय रक्षसां भागोसि॥ यजु. २.२३
‘‘सुख- शान्ति चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नहीं करता। जो यज्ञ को छोड़ता है, उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी छोड़ देते हैं। सबकी उन्नति के लिये आहुतियाँ यज्ञ में छोड़ी जाती हैं; जो आहुति नहीं छोड़ता, वह राक्षस हो जाता है।’’
यज्ञेन पापै: बहुभिर्विमुक्त: प्राप्रोति लोकान् परमस्य विष्णो:। -हारीत
‘‘यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक की भी प्राप्ति होती है।’’
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धनार्थी लभते धनम्।
भार्यार्थी शोभनां भार्यां कुमारी च शुभं पतिम्॥
भ्रष्ट राज्यस्तथा राज्यं श्रीकाम: श्रियमाप्रुयात्।
यं यं प्रार्थयते कामं स वै भवति पुष्कल:॥
निष्काम: कुरुते यस्तु स परंब्रह्म गच्छति। —मत्स्यपुराण ९३/११७- ११८
यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, विवाहार्थी को सुन्दर भार्या, कुमारी को सुन्दर पति, श्री कामना वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है और निष्काम भाव से यज्ञानुष्ठन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है।
न तस्य ग्रहपीडा स्यान्नच बन्धु- धनक्षय:।
ग्रह यज्ञ व्रतं गेहे लिखितं यत्र तिष्ठन्ति
न तत्र पीडा पापानां न रोगो न च बन्धनम्।
अशेष- यज्ञ -कोटि होम पद्धति
यज्ञ करने वाले को ग्रह पीड़ा, बन्धु नाश, धन क्षय, पाप, रोग, बन्धन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यज्ञ का फल अनन्त है।
देवा: सन्तोषिता यज्ञैर्लोकान् सम्बन्धयन्त्युत।
उभयोर्लोकयोर्देव भूतिर्यज्ञ: प्रदृश्यते॥
तस्माद्यद् याति देवत्वं पूर्वजै: सह मोदते।
नास्ति यज्ञ समं दानं नास्ति यज्ञ समो विधि:॥
सर्वधर्म समुद्देश्यो देवयज्ञे समाहित:॥
‘‘यज्ञों से सन्तुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ द्वारा लोक- परलोक का सुख प्राप्त हो सकता है। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि- विधान नहीं; यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है।’’
असुराश्च सुराश्चैव पुण्यहेतोर्मख- क्रियाम्।
प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्यज्ञा:परायणा:।
यज्ञैरेव महात्मानो बभूवुरधिका: सुरा:॥ महाभारत आश्व० ३.६,७
‘‘असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिये प्रयत्न करते हैं। सत्पुरुषों को सदा यज्ञपरायण होना चाहिये। यज्ञों से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने हैं।’’
यदिक्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।
तमाहरामि निर्ऋते रुपस्थादस्पार्शमेनं शत- शारदाय॥ -अथर्व० ३/११/२
‘‘यदि रोगी अपनी जीवनी शक्ति को खो भी चुका हो, निराशाजनक स्थिति को पहुँच गया हो, यदि मरणकाल भी समीप आ पहुँचा हो, तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है और सौ वर्ष जीवित रहने के लिये पुन: बलवान् बना देता है।’’
यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्टयुत्सर्गेण वै प्रजा:।
आप्यायन्ते तु धर्मज्ञ! यज्ञा: कल्याण- हेतव:॥ -विष्णु पुराण
‘‘यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है। यज्ञ द्वारा वर्षा होती है। वर्षा से अन्न और प्रजापालन होता है। हे धर्मज्ञ! यज्ञ ही कल्याण का हेतु है।’’
प्रयुक्तया यया चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जित:।
तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्॥ -चरक चि० खण्ड ८/११२
‘‘तपेदिक सरीखे रोगों को प्राचीनकाल में यज्ञ के प्रयोगों से नष्ट किया जाता था। रोगमुक्ति की इच्छा रखने वालों को चाहिये कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय लें।’’
अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्रिरहं हुतम्॥ -गीता ९/१६
‘‘मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ और मन्त्र, घृत, अग्रि तथा हवन भी मैं ही हूँ।’’
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य: कुरुसत्तम। -गीता ४/३१
‘‘हे अर्जुन! यज्ञरहित मनुष्य को इस लोक में भी सुख नहीं मिल सकता, फिर परलोक का सुख तो होगा ही कैसे?’’
नास्ति अयज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते शुभम्।
अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यतिच्छिन्नपर्णवत्॥ -शंख स्मृति
‘‘यज्ञ न करने वाला मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखों से वंचित हो जाता है। यज्ञ न करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती और वह पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट हो जाता है।’’
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्व पुरोवाच प्रजापति:।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:।
परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ॥
इष्टन्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:। -गीता ३/१०- ११
‘‘ब्रह्मजी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी। यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं की पुष्टि करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने- अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किये हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख- शान्ति की वस्तुयें प्रदान करेंगे।’’
असंख्यों शास्त्र वचनों में से कुछ प्रमाण ऊपर दिये गये हैं। इनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्वकाल में आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े- बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वारा यज्ञ किये जाते थे, राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे, साधारण गृहस्थ अपनी- अपनी सामर्थ्यों के अनुसार समय- समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर लोग सदैव यज्ञों को विध्वंस करने का प्रयत्न इसलिये किया करते थे कि उनके शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष न होने पाये। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का विध्वंस भी कराया गया है। रामायण में राक्षसों के ऐसे यज्ञ का वर्णन है, जिसे हनुमान् जी ने नष्ट किया था। यदि वह सफल हो जाता, तो राक्षस अजेय हो जाते।
राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके चार पुत्र पाये थे। राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इन्द्रासन के अधिकारी हुए थे। राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा सन्तान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। इन्द्र ने स्वयं भी यज्ञों द्वारा ही स्वर्ग पाया था। भगवान् राम अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया था। श्रीकृष्ण जी की प्रेरणा से पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें श्रीकृष्ण जी ने आगन्तुकों के स्वागत- सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। पापों के प्रायश्चित्त स्वरूप, अनिष्टों और प्रारब्धजन्य दुर्भाग्यों की शान्ति के निमित्त, किसी अभाव की पूर्ति के लिये, कोई सहयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से, रोग निवारणार्थ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, धन- धान्य की अधिक उपज के लिये अमृतमयी वर्षा के निमित्त, वायु मण्डल में से अस्वास्थ्यकर तत्त्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन- यज्ञ किये जाते थे और उनका परिणाम भी वैसा ही होता था।
यज्ञ एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की समिधायें काम में ली जाती हैं, उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिये किस प्रकार की हव्य वस्तुयें होमी जाती हैं, उनका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमण्डल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेदमन्त्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं, उन पर तथा निकटवर्ती वायुमण्डल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अन्तराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं, उन्हें देवता कहते हैं। उन देवताओं को अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा में प्रयोग करना, उनसे सम्बन्ध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न करना है। यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है।
संसार में कभी भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूपान्तर होता रहता है। जो वस्तुएँ हवन में होमी जाती हैं, वे तथा वेदमन्त्रों की शक्ति के साथ जो सद्भावनाएँ यज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, वे दोनों मिलकर आकाश में छा जाती हैं। उनका प्रवाह समस्त संसार के लिए कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार यह संसार की सेवा का, विश्व में सुख- शान्ति उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य परमार्थ है। यज्ञ से याज्ञिक की आत्मशुद्धि होती है, उनके पाप- ताप नष्ट होते हैं तथा शान्ति एवं सद्गति उपलब्ध होती है। सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले मनुष्यों का लोक- परलोक सुधरता है। यदि उनका पुण्य पर्याप्त हुआ, तब तो उन्हें स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा यदि दूसरा जन्म भी लेना पड़ा, तो सुखी, श्रीमान्, साधन- सम्पन्न उच्च परिवार में जन्म होता है, ताकि आगे के लिए वह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुआ लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।
यज्ञ का अर्थ- दान, एकता, उपासना से है। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन, शक्तिशाली मन्त्रों का विधिवत् उच्चारण, विधिपूर्वक बनाये हुए कुण्ड, शास्त्रोक्त समिधाएँ तथा सामग्रियाँ जब ठीक विधानपूर्वक हवन की जाती हैं, तो उनका दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मण्डल में फैल जाता है। उसके प्रभाव के फलस्वरूप प्रजा के अन्त:करण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों एवं सद्विचारों का स्वयमेव आविर्भाव होने लगता है। पत्तों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के स्थान पर जो सन्तान पैदा होती है, वह स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है। पूर्वकाल में पुत्र प्राप्ति के लिए ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हों, सो बात नहीं; जिनको बराबर सन्तानें प्राप्त होती थीं, वे भी सद्गुणी एवं प्रतिभावान सन्तान प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे। गर्भाधान, सीमान्त, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि संस्कार बालक के जन्म लेते- लेते अबोध अवस्था में ही हो जाते थे। इनमें से प्रत्येक में हवन होता था, ताकि बालक के मन पर दिव्य प्रभाव पड़ें और वह बड़ा होने पर पुरुष सिंह एवं महापुरुष बने। प्राचीनकाल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों और बुरी आदतों से ग्रसित बालकों से ही हमारे घर भरे हुए हैं।
यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत् तरंगें फैलती हैं, वे लोगों के मनों से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती हैं। फलस्वरूप उससे अनेकों समस्याएँ हल होती हैं; अनेकों उलझनें, गुत्थियाँ, पेचीदगियाँ, चिन्ताएँ, भय, आशंकाएँ तथा बुरी सम्भावनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं। राजा, धनी, सम्पन्न लोग, ऋषि- मुनि बड़े- बड़े यज्ञ करते थे, जिससे दूर- दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयाँ तथा उलझनें सुलझती थीं।
बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है। उसमें जो कुछ खिलाया जाता है, वह सच्चे अर्थों में ब्रह्मभोज है। ब्रह्म अर्थात् परमात्मा, भोज अर्थात् भोजन; परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोडऩा ही है। भगवान् हम सबको खिलाता है। हमारा भी कर्त्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी न करें। जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वे कई व्यक्ति थोड़ा- थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ साधन सुयोग न हों, वहाँ यदा- कदा छोटे- छोटे हवन किये जा सकते हैं अथवा जहाँ नियमित यज्ञ होते हैं, वहाँ अपनी ओर से कुछ आहुतियों का हवन कराया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति यज्ञ कर रहे हों, तो उसमें समय, सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न भी यज्ञ में भागीदार होना ही है।
हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यज्ञ में जो कुछ धन, सामग्री, श्रम लगाया जाता है, वह कभी निरर्थक नहीं जाता। एक प्रकार से वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है और उचित अवसर पर सन्तोषजनक ब्याज समेत वापस मिल जाता है। विधिपूर्वक शास्त्रीय पद्धति और विशिष्ट उपचारों तथा विधानों के साथ किये गये हवन तो और भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। वे एक प्रकार से दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। पूर्वकाल में यज्ञ के द्वारा मनोवाँछित वर्षा होती थी, योद्धा लोग युद्ध में विजयश्री प्राप्त करते थे और योगी आत्मसाक्षात्कार करते थे। यज्ञ को वेदों में ‘कामधुक्’ कहा है, जिसका आशय यही है कि वह मनुष्य के सभी अभावों और बाधाओं को दूर करने वाला है।
नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। उसमें कुछ इतना भारी खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा न सके। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते, वे सप्ताह में एक बार रविवार या अमावस्या, पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। विधि- विधान भी इन साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है। ‘गायत्री यज्ञ विधान’ पुस्तक में उसकी सरल विधियाँ बताई जा चुकी हैं। उनके आधार पर बिना पण्डित- पुरोहित की सहायता के कोई भी द्विज आसानी से वह करा सकता है। जहाँ कुछ भी विधान न मालूम हो, वहाँ केवल शुद्ध घृत की आहुतियाँ गायत्री मन्त्र के अन्त में ‘स्वाहा’ शब्द लगाते हुए दी जा सकती हैं। किसी न किसी रूप में यज्ञ परम्परा को जारी रखा जाए, तो वह भारतीय संस्कृति की एक बड़ी भारी सेवा है।
साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है। उससे घर की वायु शुद्धि, रोग- निवृत्ति एवं अनिष्टों से आत्मरक्षा होती है। फिर विशेष आयोजन के साथ विधि- विधानपूर्वक किये गये यज्ञ तो असाधारण फल उत्पन्न करते हैं। यह एक विद्या है। पाँचों तत्त्वों के होम में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है जिससे एक प्रचण्ड शक्ति को ‘‘द्वि मूर्धा, द्वि नासिका, सप्तहस्त, द्वि मुख, सप्तजिह्व, उत्तर मुख, कोटि द्वादश मूर्धा, द्वि पंचाशत्कला युतम्’’ आदि विशेषण युक्त कहा गया है। इस रहस्यपूर्ण संकेत में यह बताया गया है कि यज्ञाग्रि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। ये क्षेत्र सफल बनाये जा सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिका हैं, उन पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सातों प्रकार की सम्पदायें यज्ञाग्रि के हाथ में हैं, वाममार्ग और दक्षिणमार्ग ये दो मुख हैं, सातों लोक जिह्वयें हैं। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएँ हैं, वे यज्ञाग्रि के मुख में मौजूद हैं। उत्तर ध्रुव का चुम्बकत्व केन्द्र अग्रि मुख है। ५२ कलायें यज्ञ की ऐसी हैं, जिनमें से कुछ को ही प्राप्त करके रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि यह सभी कलायें उपलब्ध हो जाएँ, तो मनुष्य साक्षात् अग्रि स्वरूप हो सकता है और विश्व के सभी पदार्थ उसके करतलगत हो सकते हैं। यज्ञ की महिमा अनन्त है और उसका आयोजन भी फलदायक होता है। गायत्री उपासकों के लिए तो यज्ञ पिता तुल्य पूजनीय है। यज्ञ भगवान् की पूजा होती रहे, यह प्रयत्न करना आवश्यक है।
इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं
मन्त्रों की साधना की एक विशेष विधि- व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्मकाण्ड के अनुसार मन्त्रों का अनुष्ठान साधन, पुरश्चरण करना होता है। आमतौर से अविधिपूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उससे अनिष्ट की सम्भावना रहती है।
ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मन्त्र या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तान्त्रिक अनुष्ठान किया, पर साधना की नीति- रीति में कोई भूल हो गयी या किसी प्रकार अनुष्ठान खण्डित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पडऩा पड़ा। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी हैं। वृत्र और इन्द्र की कथा इसी प्रकार की है। वेदमन्त्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था।
अन्य वेदमन्त्रों की भाँति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधिपूर्वक साधना करना उचित है। विधिपूर्वक किये हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेदमाता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर हानिकारक फल नहीं होता।
जिस प्रकार दयालु, उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हितचिन्तना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधक का हित ही सम्पादन होता है। माता के प्रति बालक गलतियाँ भी करते रहते हैं, उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उलटा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता न तो उनके प्रति दुर्भाव मन में लाती है और न उन्हें किसी प्रकार हानि पहुँचाती है। जब साधारण माताएँ इतनी दयालुता और क्षमा प्रदर्शित करती हैं, तो जगज्जननी वेदमाता, सद्गुणों की दिव्य सुरसरि गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। वह अपने बालकों की अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती है। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है। उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरिणी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रवाह में साधना की छोटी- मोटी भूलें, कर्मकाण्ड में हुई अज्ञानवश त्रुटियाँ तिनके के समान बह जाती हैं। सतोगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में दिखाया है—
नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ —श्रीमद्भगवद्गीता २/४०
अर्थात्- सत्कार्य के आरम्भ का नाश नहीं होता, वह गिरता- पड़ता आगे बढ़ता चलता है। उससे उलटा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता की सत् इच्छा से किया हुआ कार्य असत् जो जाए और उसका शुभ परिणाम न निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है।
गायत्री साधना ऐसा ही सात्त्विक सत्कर्म है, जिसे एक बार आरम्भ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियाँ उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती हैं और बीच में छूट जाए तो फिर भी समय- समय पर बार- बार उसे पुन: आरम्भ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है, तो उसे बार- बार प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार- बार मचलती है, बार- बार चीख- पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाये तो भी उलटा परिणाम नहीं निकलता, किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक यह कि वह निष्फल चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से रूप में प्रारम्भ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है, जो अन्य उपायों से बड़ी कठिनाइयों से हटाये या मिटाये जा सकते हैं।
इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के बारहवें स्कन्द में नारद जी ने भगवान् नारायण से यही प्रश्र किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बतायें, जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सकें और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे; क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्राय: आचार- विचार, विधि- विधान, त्याग- तपस्या के कठिन नियम बतलाये गये हैं, जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या- बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान् ने कहा- ‘हे नारद! मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या न करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं, वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे महामुनि! जो सन्ध्या में अघ्र्य देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का तीन हजार जप करते हैं, वे देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं।
जप करने से पहले इसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि ‘देवो भूत्वा देवं यजेत्’ अर्थात्- ‘देव जैसा बनकर देवों का यजन करना।’ परन्तु कठिनाई या प्रमाद से न्यास न कर सके और सच्चिदानन्द गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे, तो भी पर्याप्त है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर, ब्रह्म, सूर्य, चन्द्र आदि के साथ स्पर्धा करता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है, वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।’ इस कथानक से विदित होता है कि इस युग में गायत्री की सात्त्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे निश्चित रूप से आत्मकल्याण होता है।
इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोडक़र गायत्री की उपासना करनी चाहिये। यह साधारण अस्त्र नहीं है, जिसके लिये नियत भूमिका बाँधे बिना काम न चले। मनुष्य यदि किन्हीं छुट्टल, वन- चर जीवों को पकडऩा चाहे, तो उसके लिये चतुरतापूर्ण उपायों की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु बछड़ा अपनी माँ को पकडऩा चाहे, तो उसे मातृभावना से ‘माँ’ पुकार देना काफी होता है। गौ- माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों से दुग्धपान कराने लगती है। आइये, हम भी वेदमाता को सच्चे अन्त:करण से भक्तिभावना के साथ पुकारें और उसके अन्तराल से निकला हुआ अमृत रस पान करें।
हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिये। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन? अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके प्रति श्रद्धा- भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बने पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिये, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिये कि ‘किचित् मात्र भूल हो गयी, तो बुरा होगा।’ इस भय के कारण गायत्री साधना से वञ्चित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेदमाता अपने भक्तों की भक्ति- भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती हैं और अज्ञानवश हुई छोटी- मोटी भूलों को क्षमा कर देती हैं।
साधकों के लिये कुछ आवश्यक नियम
गायत्री साधना करने वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारियाँ नीचे दी जाती हैं—
जिस प्रकार दयालु, उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हितचिन्तना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधक का हित ही सम्पादन होता है। माता के प्रति बालक गलतियाँ भी करते रहते हैं, उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उलटा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता न तो उनके प्रति दुर्भाव मन में लाती है और न उन्हें किसी प्रकार हानि पहुँचाती है। जब साधारण माताएँ इतनी दयालुता और क्षमा प्रदर्शित करती हैं, तो जगज्जननी वेदमाता, सद्गुणों की दिव्य सुरसरि गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। वह अपने बालकों की अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती है। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है। उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरिणी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रवाह में साधना की छोटी- मोटी भूलें, कर्मकाण्ड में हुई अज्ञानवश त्रुटियाँ तिनके के समान बह जाती हैं। सतोगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में दिखाया है—
नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ —श्रीमद्भगवद्गीता २/४०
अर्थात्- सत्कार्य के आरम्भ का नाश नहीं होता, वह गिरता- पड़ता आगे बढ़ता चलता है। उससे उलटा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता की सत् इच्छा से किया हुआ कार्य असत् जो जाए और उसका शुभ परिणाम न निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है।
गायत्री साधना ऐसा ही सात्त्विक सत्कर्म है, जिसे एक बार आरम्भ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियाँ उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती हैं और बीच में छूट जाए तो फिर भी समय- समय पर बार- बार उसे पुन: आरम्भ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है, तो उसे बार- बार प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार- बार मचलती है, बार- बार चीख- पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाये तो भी उलटा परिणाम नहीं निकलता, किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक यह कि वह निष्फल चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से रूप में प्रारम्भ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है, जो अन्य उपायों से बड़ी कठिनाइयों से हटाये या मिटाये जा सकते हैं।
इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के बारहवें स्कन्द में नारद जी ने भगवान् नारायण से यही प्रश्र किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बतायें, जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सकें और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे; क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्राय: आचार- विचार, विधि- विधान, त्याग- तपस्या के कठिन नियम बतलाये गये हैं, जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या- बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान् ने कहा- ‘हे नारद! मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या न करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं, वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे महामुनि! जो सन्ध्या में अघ्र्य देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का तीन हजार जप करते हैं, वे देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं।
जप करने से पहले इसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि ‘देवो भूत्वा देवं यजेत्’ अर्थात्- ‘देव जैसा बनकर देवों का यजन करना।’ परन्तु कठिनाई या प्रमाद से न्यास न कर सके और सच्चिदानन्द गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे, तो भी पर्याप्त है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर, ब्रह्म, सूर्य, चन्द्र आदि के साथ स्पर्धा करता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है, वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।’ इस कथानक से विदित होता है कि इस युग में गायत्री की सात्त्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे निश्चित रूप से आत्मकल्याण होता है।
इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोडक़र गायत्री की उपासना करनी चाहिये। यह साधारण अस्त्र नहीं है, जिसके लिये नियत भूमिका बाँधे बिना काम न चले। मनुष्य यदि किन्हीं छुट्टल, वन- चर जीवों को पकडऩा चाहे, तो उसके लिये चतुरतापूर्ण उपायों की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु बछड़ा अपनी माँ को पकडऩा चाहे, तो उसे मातृभावना से ‘माँ’ पुकार देना काफी होता है। गौ- माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों से दुग्धपान कराने लगती है। आइये, हम भी वेदमाता को सच्चे अन्त:करण से भक्तिभावना के साथ पुकारें और उसके अन्तराल से निकला हुआ अमृत रस पान करें।
हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिये। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन? अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके प्रति श्रद्धा- भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बने पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिये, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिये कि ‘किचित् मात्र भूल हो गयी, तो बुरा होगा।’ इस भय के कारण गायत्री साधना से वञ्चित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेदमाता अपने भक्तों की भक्ति- भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती हैं और अज्ञानवश हुई छोटी- मोटी भूलों को क्षमा कर देती हैं।
साधकों के लिये कुछ आवश्यक नियम
गायत्री साधना करने वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारियाँ नीचे दी जाती हैं—
१- शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिये। साधारणत: स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु- प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ- मुँह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है।
२- साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिये। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कम्बल आदि ओढक़र शीत- निवारण कर लेना उत्तम है।
३- साधना के लिए एकान्त खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूँढऩी चाहिये, जहाँ का वातावरण शान्तिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव- मन्दिर साधना के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो, वहाँ घर का कोई स्वच्छ और शान्त भाग भी चुना जा सकता है।
२- साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिये। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कम्बल आदि ओढक़र शीत- निवारण कर लेना उत्तम है।
३- साधना के लिए एकान्त खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूँढऩी चाहिये, जहाँ का वातावरण शान्तिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव- मन्दिर साधना के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो, वहाँ घर का कोई स्वच्छ और शान्त भाग भी चुना जा सकता है।
४- धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है।
५- पालथी मारकर सीधे- सादे ढंग से बैठना चाहिये। कष्टसाध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार- बार उचटता है, इसलिये इस तरह बैठना चाहिये कि देर तक बैठे रहने में असुविधा न हो।
६- रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिये। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदण्ड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है।
७- बिना बिछाये जमीन पर साधना के लिए न बैठना चाहिये। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली सारी विद्युत् जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों से बने फर्श सबसे अच्छे हैं। इनके बाद सूती आसनों का नम्बर है। ऊन तथा चर्मों के आसन तान्त्रिक कर्मां में प्रयुक्त होते हैं।
८- माला तुलसी या चन्दन की लेनी चाहिये। रुद्राक्ष, लाल चन्दन, शंख आदि की माला गायत्री के तान्त्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती हैं।
९- प्रात:काल २ घण्टे तडक़े से जप प्रारम्भ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने से एक घण्टे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिये। एक घण्टा शाम का, २ घण्टे प्रात:काल के, कुल ३ घण्टों को छोडक़र रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिणमार्गी साधना नहीं करनी चाहिये। तान्त्रिक साधनाएँ अर्ध रात्रि के आस- पास की जाती हैं।
१०- साधना के लिए चार बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये— (अ) चित्त एकाग्र रहे, मन इधर- उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े, तो उसे माता की सुन्दर छवि के ध्यान में लगाना चाहिये। (ब) माता के प्रति अगाध श्रद्धा व विश्वास हो। अविश्वासी और शंका- शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। (स) दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिये। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्र हैं। इन विघ्रों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बढ़ते चलना चाहिये। (द) निरन्तरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यन्त कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही, पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिये। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करना चाहिये। समय को रोज- रोज नहीं बदलना चाहिये। कभी सबेरे, कभी दोपहर, कभी तीन बजे तो कभी दस बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन चार नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है।
११- कम से कम एक माला अर्थात् १०८ मन्त्र नित्य जपने चाहिये, इससे अधिक जितने बन पड़े, उतने उत्तम हैं।
१२- किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना- गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिये। अपने लिए कौन- सी साधना उपयुक्त है, इसका निर्णय उसी से कराना चाहिये। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाला, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाला साधना- गुरु होना अति आवश्यक है।
१३- प्रात:काल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिये और शाम को पश्चिम की ओर मुँह करके। प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुँह करना उचित है।
१४- पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिये। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो, तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेंहदी के देशी रंगों से रँगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए।
१५- देर तक एक पालथी से, एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे- बैठे पैर थक जाएँ, तब उन्हें बदला जा सकता है। आसन बदलने में दोष नहीं।
१६- मल- मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिये साधना के बीच उठना पड़े, तो शुद्ध जल से हाथ- मुँह धोकर दुबारा बैठना चाहिये और विक्षेप के लिए एक माला अतिरिक्त जप प्रायश्चित्त स्वरूप करना चाहिये।
१७- यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े, तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दण्ड स्वरूप करना चाहिये।
१८- जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत् जप स्थगित रखना चाहिये। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर सवालक्ष जप के अनुष्ठान काल में आ जाए, तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर उसी संख्या पर से जप आरम्भ किया जा सकता है, जहाँ से छोड़ा था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए एक हजार जप विशेष रूप से करना चाहिये।
१९- लम्बे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े- पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है।
२०- साधक का आहार- विहार सात्त्विक होना चाहिये। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाये हुए पदार्थ होने चाहिये। अधिक मिर्च- मसाले, तले हुए पक्वान्न, मिष्ठान्न, बासी, दुर्गन्धित, मांस, नशीली, अभक्ष्य, उष्ण, दाहक, अनीति उपार्जित, गन्दे मनुष्यों द्वारा बनाये हुए, तिरस्कार पूर्वक दिये हुए भोजन से जितना बचा जा सके, उतना ही अच्छा है।
२१- व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म- संगत, सरल एवं सात्त्विक रह सके, उतना ही उत्तम है। फैशनपरस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच- रंग अधिक देखना, पर निन्दा, छिद्रान्वेषण, कलह, दुराचार, ईष्र्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर से जितना बचा जा सके, बचने का प्रयत्न करना चाहिये।
२२- यों ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के ४० दिन में उसकी विशेष आवश्यकता है।
२३- अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं- (१) ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल न कटाएँ, ठोड़ी के बाल अपने हाथों से ही बनायें। (२) चारपाई पर न सोयें, तख्त या जमीन पर सोना चाहिये। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैरों न फिरें। चाम के जूते के स्थान पर खड़ाऊ आदि का उपयोग करना चाहिये। (४) इन दिनों एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिये। (५) अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें।
२४- एकान्त में जपते समय माला खुले में जपनी चाहिये। जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो, वहाँ कपड़े से ढक लेना चाहिये या गोमुखी में हाथ डाल लेना चाहिये।
२५- साधना के दौरान पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यों ही जहाँ- तहाँ ऐसी जगह नहीं फेंक देनी चाहिये, जहाँ वे पैरों तले कुचलती फिरे। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव- मन्दिर, कपास, जौ, चावल का खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिये। चावल चिडिय़ों के लिए डाल देना चाहिये। नैवेद्य आदि बालकों को बाँट देने चाहिये। जल को सूर्य के सम्मुख अघ्र्य देना चाहिये।
२६- वेदोक्त रीति की यौगिक दक्षिणमार्गी क्रियाओं में और तन्त्रोक्त वाममार्गी क्रियाओं में अन्तर है। योगमार्गी सरल विधियाँ इस पुस्तक में लिखी हुई हैं, उनमें कोई विशेष कर्मकाण्ड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला, मुद्रा, अंग न्यास आदि कर्मकाण्ड तान्त्रिक साधनाओं के लिये हैं। इस पुस्तक के आधार पर साधना करने वालों को उसकी आवश्यकता नहीं है।
२७- प्रचलित शास्त्रीय मान्यता के अनुसार गायत्री का अधिकार द्विजों को है। द्विज का अर्थ होता है जिनका दूसरा जन्म हुआ है। गायत्री की दीक्षा लेने वालों को ही द्विज कहते हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है जिसे गीता में गुण- कर्म के अनुसार निर्धारित करने का अनुशासन बतलाया गया है। जन्म से वर्ण निर्धारित करने पर उन्हें जाति कहा जाने लगा। वास्तव में शूद्र उन्हें कहा जाता था जो द्विजत्व का संस्कार स्वीकार नहीं करते थे। गुण- कर्म के आधार पर धीवर कन्या के गर्भ से उत्पन्न बालक महर्षि व्यास, इतरा का बेटा ऋषि ऐतरेय बनने जैसे अनेक उदाहरण पौराणिक इतिहास में मिलते हैं।
२८- वेद मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिये जप इस प्रकार प्रकार करना चाहिए कि कण्ठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मन्त्र को न सुन सके। इस प्रकार किया जप स्वर- बन्धनों से मुक्त होता है।
२९- साधना की अनेक विधियाँ हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो कुछ न कुछ मीन- मेख निकाल कर सन्देह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे, इसलिये अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिये। यदि दूसरे मतभेद प्रकट करें, तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिये। यदि कोई दोष की बात होगी, तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पड़ेगा। साधक तो निर्दोष और श्रद्धायुक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पायेगा। वाल्मीकि जी उलटा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो गये थे।
३०- गायत्री साधना माता की चरण- वन्दना के समान है, यह कभी निष्फल नहीं होती, उलटा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं, इसलिये निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिये। अन्य मन्त्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्वसुलभ, अत्यन्त सुगम और सब प्रकार सुसाध्य है। हाँ, तान्त्रिक विधि से की गयी उपासना पूर्ण विधि- विधान के साथ होनी चाहिये, उसमें अन्तर पडऩा हानिकारक है।
३१- जैसे मिठाई को अकेले- अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुम्बियों को उसके लिये प्रोत्साहित न करना, एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिये कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करें।
३२- कोई बात समझ में न आती हो या सन्देह हो तो ‘शांतिकुञ्ज हरिद्वार’ से उसका समाधान कराया जा सकता है।
३३- माला जपते समय सुमेरु (माला के आरम्भ का सबसे बड़ा दाना) का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उलटा ही वापस कर लेना चाहिये। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरम्भ करना चाहिये। अपनी पूजा- सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिये, जिसे अन्य लोग अधिक स्पर्श न करें।
५- पालथी मारकर सीधे- सादे ढंग से बैठना चाहिये। कष्टसाध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार- बार उचटता है, इसलिये इस तरह बैठना चाहिये कि देर तक बैठे रहने में असुविधा न हो।
६- रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिये। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदण्ड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है।
७- बिना बिछाये जमीन पर साधना के लिए न बैठना चाहिये। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली सारी विद्युत् जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों से बने फर्श सबसे अच्छे हैं। इनके बाद सूती आसनों का नम्बर है। ऊन तथा चर्मों के आसन तान्त्रिक कर्मां में प्रयुक्त होते हैं।
८- माला तुलसी या चन्दन की लेनी चाहिये। रुद्राक्ष, लाल चन्दन, शंख आदि की माला गायत्री के तान्त्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती हैं।
९- प्रात:काल २ घण्टे तडक़े से जप प्रारम्भ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने से एक घण्टे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिये। एक घण्टा शाम का, २ घण्टे प्रात:काल के, कुल ३ घण्टों को छोडक़र रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिणमार्गी साधना नहीं करनी चाहिये। तान्त्रिक साधनाएँ अर्ध रात्रि के आस- पास की जाती हैं।
१०- साधना के लिए चार बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये— (अ) चित्त एकाग्र रहे, मन इधर- उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े, तो उसे माता की सुन्दर छवि के ध्यान में लगाना चाहिये। (ब) माता के प्रति अगाध श्रद्धा व विश्वास हो। अविश्वासी और शंका- शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। (स) दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिये। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्र हैं। इन विघ्रों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बढ़ते चलना चाहिये। (द) निरन्तरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यन्त कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही, पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिये। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करना चाहिये। समय को रोज- रोज नहीं बदलना चाहिये। कभी सबेरे, कभी दोपहर, कभी तीन बजे तो कभी दस बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन चार नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है।
११- कम से कम एक माला अर्थात् १०८ मन्त्र नित्य जपने चाहिये, इससे अधिक जितने बन पड़े, उतने उत्तम हैं।
१२- किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना- गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिये। अपने लिए कौन- सी साधना उपयुक्त है, इसका निर्णय उसी से कराना चाहिये। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाला, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाला साधना- गुरु होना अति आवश्यक है।
१३- प्रात:काल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिये और शाम को पश्चिम की ओर मुँह करके। प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुँह करना उचित है।
१४- पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिये। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो, तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेंहदी के देशी रंगों से रँगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए।
१५- देर तक एक पालथी से, एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे- बैठे पैर थक जाएँ, तब उन्हें बदला जा सकता है। आसन बदलने में दोष नहीं।
१६- मल- मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिये साधना के बीच उठना पड़े, तो शुद्ध जल से हाथ- मुँह धोकर दुबारा बैठना चाहिये और विक्षेप के लिए एक माला अतिरिक्त जप प्रायश्चित्त स्वरूप करना चाहिये।
१७- यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े, तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दण्ड स्वरूप करना चाहिये।
१८- जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत् जप स्थगित रखना चाहिये। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर सवालक्ष जप के अनुष्ठान काल में आ जाए, तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर उसी संख्या पर से जप आरम्भ किया जा सकता है, जहाँ से छोड़ा था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए एक हजार जप विशेष रूप से करना चाहिये।
१९- लम्बे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े- पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है।
२०- साधक का आहार- विहार सात्त्विक होना चाहिये। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाये हुए पदार्थ होने चाहिये। अधिक मिर्च- मसाले, तले हुए पक्वान्न, मिष्ठान्न, बासी, दुर्गन्धित, मांस, नशीली, अभक्ष्य, उष्ण, दाहक, अनीति उपार्जित, गन्दे मनुष्यों द्वारा बनाये हुए, तिरस्कार पूर्वक दिये हुए भोजन से जितना बचा जा सके, उतना ही अच्छा है।
२१- व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म- संगत, सरल एवं सात्त्विक रह सके, उतना ही उत्तम है। फैशनपरस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच- रंग अधिक देखना, पर निन्दा, छिद्रान्वेषण, कलह, दुराचार, ईष्र्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर से जितना बचा जा सके, बचने का प्रयत्न करना चाहिये।
२२- यों ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के ४० दिन में उसकी विशेष आवश्यकता है।
२३- अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं- (१) ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल न कटाएँ, ठोड़ी के बाल अपने हाथों से ही बनायें। (२) चारपाई पर न सोयें, तख्त या जमीन पर सोना चाहिये। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैरों न फिरें। चाम के जूते के स्थान पर खड़ाऊ आदि का उपयोग करना चाहिये। (४) इन दिनों एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिये। (५) अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें।
२४- एकान्त में जपते समय माला खुले में जपनी चाहिये। जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो, वहाँ कपड़े से ढक लेना चाहिये या गोमुखी में हाथ डाल लेना चाहिये।
२५- साधना के दौरान पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यों ही जहाँ- तहाँ ऐसी जगह नहीं फेंक देनी चाहिये, जहाँ वे पैरों तले कुचलती फिरे। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव- मन्दिर, कपास, जौ, चावल का खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिये। चावल चिडिय़ों के लिए डाल देना चाहिये। नैवेद्य आदि बालकों को बाँट देने चाहिये। जल को सूर्य के सम्मुख अघ्र्य देना चाहिये।
२६- वेदोक्त रीति की यौगिक दक्षिणमार्गी क्रियाओं में और तन्त्रोक्त वाममार्गी क्रियाओं में अन्तर है। योगमार्गी सरल विधियाँ इस पुस्तक में लिखी हुई हैं, उनमें कोई विशेष कर्मकाण्ड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला, मुद्रा, अंग न्यास आदि कर्मकाण्ड तान्त्रिक साधनाओं के लिये हैं। इस पुस्तक के आधार पर साधना करने वालों को उसकी आवश्यकता नहीं है।
२७- प्रचलित शास्त्रीय मान्यता के अनुसार गायत्री का अधिकार द्विजों को है। द्विज का अर्थ होता है जिनका दूसरा जन्म हुआ है। गायत्री की दीक्षा लेने वालों को ही द्विज कहते हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है जिसे गीता में गुण- कर्म के अनुसार निर्धारित करने का अनुशासन बतलाया गया है। जन्म से वर्ण निर्धारित करने पर उन्हें जाति कहा जाने लगा। वास्तव में शूद्र उन्हें कहा जाता था जो द्विजत्व का संस्कार स्वीकार नहीं करते थे। गुण- कर्म के आधार पर धीवर कन्या के गर्भ से उत्पन्न बालक महर्षि व्यास, इतरा का बेटा ऋषि ऐतरेय बनने जैसे अनेक उदाहरण पौराणिक इतिहास में मिलते हैं।
२८- वेद मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिये जप इस प्रकार प्रकार करना चाहिए कि कण्ठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मन्त्र को न सुन सके। इस प्रकार किया जप स्वर- बन्धनों से मुक्त होता है।
२९- साधना की अनेक विधियाँ हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो कुछ न कुछ मीन- मेख निकाल कर सन्देह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे, इसलिये अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिये। यदि दूसरे मतभेद प्रकट करें, तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिये। यदि कोई दोष की बात होगी, तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पड़ेगा। साधक तो निर्दोष और श्रद्धायुक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पायेगा। वाल्मीकि जी उलटा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो गये थे।
३०- गायत्री साधना माता की चरण- वन्दना के समान है, यह कभी निष्फल नहीं होती, उलटा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं, इसलिये निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिये। अन्य मन्त्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्वसुलभ, अत्यन्त सुगम और सब प्रकार सुसाध्य है। हाँ, तान्त्रिक विधि से की गयी उपासना पूर्ण विधि- विधान के साथ होनी चाहिये, उसमें अन्तर पडऩा हानिकारक है।
३१- जैसे मिठाई को अकेले- अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुम्बियों को उसके लिये प्रोत्साहित न करना, एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिये कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करें।
३२- कोई बात समझ में न आती हो या सन्देह हो तो ‘शांतिकुञ्ज हरिद्वार’ से उसका समाधान कराया जा सकता है।
३३- माला जपते समय सुमेरु (माला के आरम्भ का सबसे बड़ा दाना) का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उलटा ही वापस कर लेना चाहिये। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरम्भ करना चाहिये। अपनी पूजा- सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिये, जिसे अन्य लोग अधिक स्पर्श न करें।
Versions
-

ENGLISHSuper Science of GayatriScan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानScan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 1Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 2Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 3Scan Book Version
-
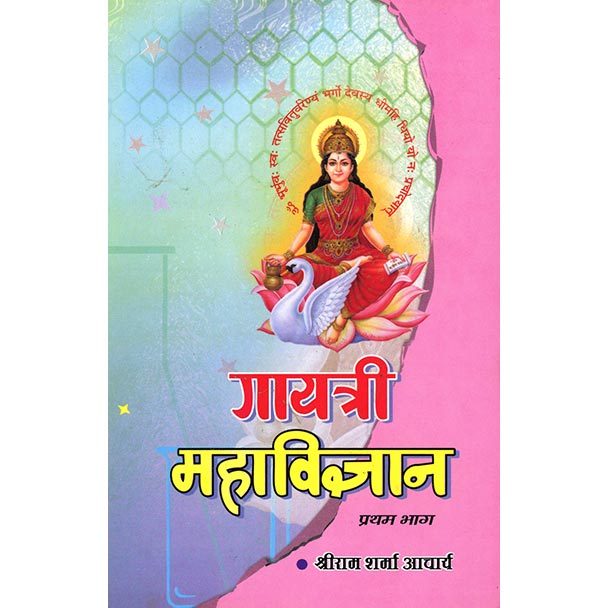
MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग १Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग २Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग ३Scan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानText Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग)Text Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान भाग 2Text Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री महाविज्ञान भाग १
- वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति
- ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव
- गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है
- गायत्री साधना से शक्तिकोशों का उद्भव
- शरीर में गायत्री मंत्र के अक्षर
- गायत्री और ब्रह्म की एकता
- महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान
- त्रिविध दु:खों का निवारण
- गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना
- गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता
- गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण
- जीवन का कायाकल्प
- नारियों को वेद एवं गायत्री का अधिकार
- देवियों की गायत्री साधना
- गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य
- गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत (जनेऊ)
- साधकों के लिये उपवीत आवश्यक है
- गायत्री साधना का उद्देश्य
- निष्काम साधना का तत्त्व ज्ञान
- गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध
- साधना- एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- आत्मशक्ति का अकूत भण्डार :: अनुष्ठान
- सदैव शुभ गायत्री यज्ञ
- महिलाओं के लिये विशेष साधनाएँ
- एक वर्ष की उद्यापन साधना
- गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि
- गायत्री का अर्थ चिन्तन
- साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते
- साधना की सफलता के लक्षण
- सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिये
- गायत्री द्वारा कुण्डलिनी जागरण
- यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बाँटिये
- गायत्री महाविज्ञान भाग ३ भूमिका
- गायत्री के पाँच मुख
- अनन्त आनन्द की साधना
- गायत्री मञ्जरी
- अन्नमय कोश और उसकी साधना
- उपवास - अन्नमय कोश की साधना
- आसन - अन्नमय कोश की साधना
- तत्त्व शुद्धि - अन्नमय कोश की साधना
- तपश्चर्या - अन्नमय कोश की साधना
- मनोमय कोश की साधना
- ध्यान - मनोमय कोश की साधना
- त्राटक - मनोमय कोश की साधना
- जप - मनोमय कोश की साधना
- तन्मात्रा साधना - मनोमय कोश की साधना
- विज्ञानमय कोश की साधना
- सोऽहं साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मानुभूति योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मचिन्तन की साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- स्वर योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- वायु साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- ग्रन्थि-भेद - विज्ञानमय कोश की साधना
- आनन्दमय कोश की साधना
- नाद साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- बिन्दु साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- कला साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- तुरीयावस्था - आनन्दमय कोश की साधना
- पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य
- गायत्री-साधना निष्फल नहीं जाती
- पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य
- गायत्री का तन्त्रोक्त वाम-मार्ग
- गायत्री की गुरु दीक्षा
- आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- मन्त्र दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- अग्नि दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्म दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- कल्याण मन्दिर का प्रवेश द्वार - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्मदीक्षा की दक्षिणा आत्मदान - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- वर्तमानकालीन कठिनाइयाँ - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ

