गायत्री महाविज्ञान 
विज्ञानमय कोश की साधना
Read Scan Version
अन्नमय, प्राणमय और मनोमय इन तीनों कोशों के उपरान्त आत्मा का चौथा आवरण, गायत्री का चौथा मुख विज्ञानमय कोश है। आत्मोन्नति की चतुर्थ भूमिका में विज्ञानमय कोश की साधना की जाती है।
विज्ञान का अर्थ है -विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक-व्यवहार को, अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक समस्याओं को समझते हैं। स्थूल में इसी साधारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है। राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, संगीत, वक्तृत्व, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध बातों की जानकारी विविध प्रकार से की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर शरीर से सम्बन्ध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है। जिसके पास ये जानकारियाँ जितनी अधिक होंगी, जो लोक-व्यवहार में जितना अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत, यशस्वी, प्रतिष्ठित, सम्पन्न एवं ऐश्वर्यवान होगा।
किन्तु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही सीमित है। आत्मा का उससे कुछ हित सम्पादन नहीं हो सकता। देखा जाता है कि कई व्यक्ति धनवान्, प्रतिष्ठित, नेता और गुणवान् होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कई- कई मनुष्य आत्मा-परमात्मा के बारे में बहुत बातें करते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, वेदान्त, योग आदि के बारे में बहुत-सी बातें पढ़-सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं और बड़ी-बड़ी बातें बढ़-चढ़कर करते हैं तथा साथियों पर अपनी विशेषता की छाप जमाते हैं। इतना करते हुए भी वस्तुत: उनकी आत्मिक धारणाएँ बड़ी निर्बल होती हैं। श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से उनकी स्थिति साधारण लोगों से कुछ अच्छी नहीं होती।
गीता, उपनिषद्, रामायण, वेदशास्त्र आदि सद्ग्रन्थों के पढ़ने एवं सत्पुरुषों के प्रवचन सुनने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है, जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक भी है। परन्तु इन विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो ही जाए।
इसमें तो सन्देह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना, भाषा ज्ञान, शास्त्राध्ययन आदि जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं और इनके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति कबीर, रैदास और तुकाराम की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर ही आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। पर वर्तमान समय में लोगों ने भौतिक जीवन को इतना अधिक महत्त्व दे दिया है, धनोपार्जन को वे इतना सर्वोपरि गुण मानते हैं कि अध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, उलटा वे उसे अनावश्यक समझने लग जाते हैं।
इस पुस्तक के आरम्भ में वरुण और भृगु की कथा दी गई है। भृगु पूर्ण विद्वान् थे, वेद-वेदान्तों के पूरे ज्ञाता थे, फिर भी वे जानते थे कि मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए वरुण के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि ‘हे भगवान्! मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश दीजिए।’ वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और न कोई लम्बा-चौड़ा प्रवचन ही सुनाया, वरन् उन्होंने आदेश दिया—‘तप करो।’ तप करने से एक-एक कोश को पार करते हुए क्रमश: उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया। ऐसी ही अनेक कथाएँ हैं। उद्दालक ने श्वेतकेतु को, ब्रह्मा ने इन्द्र को, अंगिरा ने विवस्वान को इसी प्रकार तप करके ब्रह्म को जानने का आदेश दिया था।
ज्ञान का अभिप्राय है-जानकारी। विज्ञान का अभिप्राय है-श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु यह जानते हैं कि ‘आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानन्द स्वरूप है’, परन्तु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति भूमिका में नहीं होता। स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो जाता है। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रति क्षण होती रहती है। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। तब कैसे कहा जाए कि आत्मा की अमरता, शरीर की भिन्नता तथा ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा है, आस्था, विश्वास है?
अपने सम्बन्ध में तात्त्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतया अनुभव करना यही विज्ञान का उद्देश्य है। आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते हैं। स्थूल शरीर-से जैसे कुछ हम हैं, वही उनकी आत्म-मान्यता है। जाति, वंश, प्रदेश, सम्प्रदाय, व्यवसाय, पद, विद्या, धन, आयु, स्थिति, लिंग आदि के आधार पर वह मान्यता बनाई जाती है कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न पूछने पर कि ‘आप कौन हैं’ लोग इन्हीं बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को समझते भी वे यही हैं। इस मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थों का निर्धारण होता है। जिस स्थिति में स्वयं हैं, उसी स्थिति का अहंकार अपने में जाग्रत् होता और स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति, तुष्टि तथा सन्तुष्टि जिस प्रकार होनी सम्भव दिखाई पड़ती है, वही जीवन की अन्तरंग नीति बन जाती है।
बाहर से लोग धर्म और सदाचार की, सिद्धान्तों और आदर्शों की बातें करते रहते हैं, पर उनका अन्त:करण उसी दिशा में काम करता है जिस ओर उनकी जीवन-नीति प्रेरणा देती है। जब अपने को शरीर मान लिया गया है, तो शरीर का सुख ही अभीष्ट होना चाहिए। इन्द्रिय भोगों की, मौज-मजे की, मान-बड़ाई की, ऐश-आराम की प्राप्ति ही शरीर का सुख है। इन सुखों के लिए धन की आवश्यकता है। अस्तु, धन को अधिक से अधिक जुटाना और भोग-ऐश्वर्य में निमग्न रहना यही प्रधान कार्यक्रम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो किया जाता है, वह तो एक प्रकार की तफरीह के लिए, विनोद के लिए होता है। ऐसे लोग कभी-कभी धर्मचर्चा या पूजा-पाठ भी करते देखे जाते हैं। यह उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो आत्म-मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से आज यही भौतिक दृष्टि सर्वत्र दृष्टिगोचर है। धन और भोग की छीना-झपटी में लोग एक-दूसरे से बाजी मारने में इसी दृष्टिकोण के कारण जी-जान से जुटे हुए हैं। परिणाम स्वरूप जिन कलह-क्लेशों का सामना करना पड़ रहा है, वह सामने है।
विज्ञान इस अज्ञान रूपी अन्धकार से हमें बचाता है। जिस मनोभूमि में पहुँचकर जीव यह अनुभव करता है कि ‘मैं शरीर नहीं, वस्तुत: आत्मा ही हूँ’, उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है, तब तक वह अपने को स्त्री-पुरुष, मनुष्य, पशु, मोटा-पतला, पहलवान, काला, गोरा आदि शरीर सबन्धी भेदों से पहचानता है। जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति होती है, तो गुणों के आधार पर अपनत्व का बोध होता है। शिल्पी, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, मूर्ख, कायर, शूरवीर, लेखक, वक्ता, धनी, गरीब आदि की मान्यताएँ प्राण भूमिका में होती हैं। मनोमय कोश की स्थिति में पहुँचने पर अपने मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है। लोभी, दम्भी, चोर, उदार, विषयी, संयमी, नास्तिक, आस्तिक, स्वार्थी, परमार्थी, दयालु, निष्ठुर आदि कर्त्तव्य और धर्म की औचित्य-अनौचित्य सम्बन्धी मान्यताएँ जब अपने सम्बन्ध में बनती हों, उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुँचा हुआ है। इससे चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका है, जिसमें पहुँचकर जीव अपने को यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर से, गुणों से, स्वभाव से ऊपर हूँ; मैं ईश्वर का राजकुमार, अविनाशी आत्मा हूँ।
जीभ से अपने को आत्मा कहने वाले असंख्य लोग हैं, उन्हें आत्मज्ञानी नहीं कह सकते। आत्मज्ञानी वह है जो दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भीतर यह अनुभव करता है—‘‘मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। शरीर मेरा वाहन है। प्राण मेरा अस्त्र है। मन मेरा सेवक है। मैं इन सबसे ऊपर, इन सबसे अलग, इन सबका स्वामी आत्मा हूँ। मेरे स्वार्थ इनसे अलग हैं, मेरे लाभ और स्थूल शरीर के लाभों में, स्वार्थों में भारी अन्तर है।’’ इस अन्तर को समझकर जीव अपने लाभ, स्वार्थ, हित और कल्याण के लिए कटिबद्ध होता है, आत्मोन्नति के लिए अग्रसर होता है, तो उसे अपना स्वरूप और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है।
विज्ञानमय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुँचे हुए जीव का दृष्टिकोण सांसारिक जीवों से भिन्न होता है। गीता में योगी का लक्षण बताया गया है कि जब सब जीव सोते हैं, तब योगी जागता है और सब जीव जब जागते हैं, तब योगी सो जाता है। इन आलंकारिक शब्दों में रात को जागने और दिन में सोने का विधान नहीं है, वरन् यह बताया गया है कि जिन चीजों के लिए साधारण लोग बेतरह इच्छुक, प्यासे, लालायित, सतृष्ण और आकांक्षी रहते हैं, योगी का मन इधर से फिर जाता है; क्योंकि वह देखता है कि कामिनी और कञ्चन की माया शरीर को गुदगुदाती है, पर आत्मा को ले बैठती है। इससे क्षणिक सुख के लिए स्थिर आनन्द का नाश करना उचित नहीं है। जिन धन-सन्तान, कुटुम्ब-कबीला, शत्रु-मित्र, हानि-लाभ, आगा-पीछा, निन्दा-स्तुति आदि की समस्याओं में साधारण लोग बेतरह फँसे रहते हैं, ये बातें योगियों के लिए अबोध बच्चों की ‘बालक्रीड़ा’ से अधिक कुछ भी महत्त्व की दिखाई नहीं देतीं; इसलिए वे उनकी ओर से उदास हो जाते हैं। वे इस झमेले को बहुत कम महत्त्व देते हैं। फलस्वरूप यह समस्याएँ उनके लिए अपने आप सुलझ जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं।
जिन कार्यों में, विचारों में कामी लोग, मायाग्रस्त व्यक्ति अत्यन्त मोहग्रस्त होकर चिपके रहते हैं, उनकी ओर से योगी मुँह फेर लेते हैं। इस प्रकार वे वहाँ सोये हुए माने जाते हैं, जहाँ कि अन्य जीव जागते हैं। इसी प्रकार जिन कार्यों की ओर, संयम, त्याग, परमार्थ, आत्मलाभ की ओर सांसारिक जीवों का बिलकुल ध्यान नहीं होता, उनमें योगी दत्तचित्त होकर संलग्न रहते हैं। इस स्थिति के बारे में ही गीता में कहा गया है कि जब जीव सोते हैं, तब योगी जागते हैं।
शरीर यात्रा के लिए प्राय: सभी मनुष्यों को मिलता-जुलता कार्यक्रम रखना पड़ता है, पर योगी और भोगी के जीवन तथा रीति में भारी अन्तर होता है। प्राय: सभी लोग तड़के नित्यकर्म से निवृत होते और भोजन करके काम में लगते हैं। शाम तक जो श्रम करना पड़ता है, उसमें से अधिकांश समय अन्न, वस्त्र और जीवन आश्रितों की व्यवस्था में लग जाता है। शाम को फिर नित्यकर्म, भोजन और रात को सो जाना। इस धुरी पर सबका जीवन घूमता है, परन्तु अन्त:स्थिति में जमीन-आसमान का भेद है। एक मनुष्य अपने शरीर के लिए धन और भोग इकट्ठे करने की योजना सामने रखकर अपने हर विचार और कार्य को करता है, जबकि दूसरा अपने आत्मा को समझकर आत्मकल्याण की नीति पर चलता है। ये विभिन्न दृष्टिकोण ही एक के कामों को पुण्य एवं यज्ञ बना देते हैं और दूसरे के काम पाप एवं बन्धन बन जाते हैं।
आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, आत्मलाभ, आत्मप्राप्ति, आत्मदर्शन, आत्मकल्याण को जीवन लक्ष्य माना गया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होता है जब हमारी अन्त:चेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास-भावना के साथ यह अनुभव करे कि मैं वस्तुत: परब्रह्म परमात्मा की अविच्छिन्न अंश, अविनाशी आत्मा हूँ। इस भावना की पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्मसाक्षात्कार है।
आत्मसाक्षात्कार की चार साधनाएँ नीचे दी जाती हैं—(१) सोऽहं साधना, (२) आत्मानुभूति, (३) स्वर संयम, (४) ग्रन्थिभेद । ये चारों ही विज्ञानमय कोश को प्रबुद्ध करने वाली हैं।
विज्ञान का अर्थ है -विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक-व्यवहार को, अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक समस्याओं को समझते हैं। स्थूल में इसी साधारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है। राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, संगीत, वक्तृत्व, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध बातों की जानकारी विविध प्रकार से की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर शरीर से सम्बन्ध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है। जिसके पास ये जानकारियाँ जितनी अधिक होंगी, जो लोक-व्यवहार में जितना अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत, यशस्वी, प्रतिष्ठित, सम्पन्न एवं ऐश्वर्यवान होगा।
किन्तु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही सीमित है। आत्मा का उससे कुछ हित सम्पादन नहीं हो सकता। देखा जाता है कि कई व्यक्ति धनवान्, प्रतिष्ठित, नेता और गुणवान् होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कई- कई मनुष्य आत्मा-परमात्मा के बारे में बहुत बातें करते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, वेदान्त, योग आदि के बारे में बहुत-सी बातें पढ़-सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं और बड़ी-बड़ी बातें बढ़-चढ़कर करते हैं तथा साथियों पर अपनी विशेषता की छाप जमाते हैं। इतना करते हुए भी वस्तुत: उनकी आत्मिक धारणाएँ बड़ी निर्बल होती हैं। श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से उनकी स्थिति साधारण लोगों से कुछ अच्छी नहीं होती।
गीता, उपनिषद्, रामायण, वेदशास्त्र आदि सद्ग्रन्थों के पढ़ने एवं सत्पुरुषों के प्रवचन सुनने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है, जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक भी है। परन्तु इन विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो ही जाए।
इसमें तो सन्देह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना, भाषा ज्ञान, शास्त्राध्ययन आदि जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं और इनके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति कबीर, रैदास और तुकाराम की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर ही आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। पर वर्तमान समय में लोगों ने भौतिक जीवन को इतना अधिक महत्त्व दे दिया है, धनोपार्जन को वे इतना सर्वोपरि गुण मानते हैं कि अध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, उलटा वे उसे अनावश्यक समझने लग जाते हैं।
इस पुस्तक के आरम्भ में वरुण और भृगु की कथा दी गई है। भृगु पूर्ण विद्वान् थे, वेद-वेदान्तों के पूरे ज्ञाता थे, फिर भी वे जानते थे कि मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए वरुण के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि ‘हे भगवान्! मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश दीजिए।’ वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और न कोई लम्बा-चौड़ा प्रवचन ही सुनाया, वरन् उन्होंने आदेश दिया—‘तप करो।’ तप करने से एक-एक कोश को पार करते हुए क्रमश: उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया। ऐसी ही अनेक कथाएँ हैं। उद्दालक ने श्वेतकेतु को, ब्रह्मा ने इन्द्र को, अंगिरा ने विवस्वान को इसी प्रकार तप करके ब्रह्म को जानने का आदेश दिया था।
ज्ञान का अभिप्राय है-जानकारी। विज्ञान का अभिप्राय है-श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु यह जानते हैं कि ‘आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानन्द स्वरूप है’, परन्तु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति भूमिका में नहीं होता। स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो जाता है। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रति क्षण होती रहती है। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। तब कैसे कहा जाए कि आत्मा की अमरता, शरीर की भिन्नता तथा ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा है, आस्था, विश्वास है?
अपने सम्बन्ध में तात्त्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतया अनुभव करना यही विज्ञान का उद्देश्य है। आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते हैं। स्थूल शरीर-से जैसे कुछ हम हैं, वही उनकी आत्म-मान्यता है। जाति, वंश, प्रदेश, सम्प्रदाय, व्यवसाय, पद, विद्या, धन, आयु, स्थिति, लिंग आदि के आधार पर वह मान्यता बनाई जाती है कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न पूछने पर कि ‘आप कौन हैं’ लोग इन्हीं बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को समझते भी वे यही हैं। इस मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थों का निर्धारण होता है। जिस स्थिति में स्वयं हैं, उसी स्थिति का अहंकार अपने में जाग्रत् होता और स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति, तुष्टि तथा सन्तुष्टि जिस प्रकार होनी सम्भव दिखाई पड़ती है, वही जीवन की अन्तरंग नीति बन जाती है।
बाहर से लोग धर्म और सदाचार की, सिद्धान्तों और आदर्शों की बातें करते रहते हैं, पर उनका अन्त:करण उसी दिशा में काम करता है जिस ओर उनकी जीवन-नीति प्रेरणा देती है। जब अपने को शरीर मान लिया गया है, तो शरीर का सुख ही अभीष्ट होना चाहिए। इन्द्रिय भोगों की, मौज-मजे की, मान-बड़ाई की, ऐश-आराम की प्राप्ति ही शरीर का सुख है। इन सुखों के लिए धन की आवश्यकता है। अस्तु, धन को अधिक से अधिक जुटाना और भोग-ऐश्वर्य में निमग्न रहना यही प्रधान कार्यक्रम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो किया जाता है, वह तो एक प्रकार की तफरीह के लिए, विनोद के लिए होता है। ऐसे लोग कभी-कभी धर्मचर्चा या पूजा-पाठ भी करते देखे जाते हैं। यह उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो आत्म-मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से आज यही भौतिक दृष्टि सर्वत्र दृष्टिगोचर है। धन और भोग की छीना-झपटी में लोग एक-दूसरे से बाजी मारने में इसी दृष्टिकोण के कारण जी-जान से जुटे हुए हैं। परिणाम स्वरूप जिन कलह-क्लेशों का सामना करना पड़ रहा है, वह सामने है।
विज्ञान इस अज्ञान रूपी अन्धकार से हमें बचाता है। जिस मनोभूमि में पहुँचकर जीव यह अनुभव करता है कि ‘मैं शरीर नहीं, वस्तुत: आत्मा ही हूँ’, उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है, तब तक वह अपने को स्त्री-पुरुष, मनुष्य, पशु, मोटा-पतला, पहलवान, काला, गोरा आदि शरीर सबन्धी भेदों से पहचानता है। जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति होती है, तो गुणों के आधार पर अपनत्व का बोध होता है। शिल्पी, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, मूर्ख, कायर, शूरवीर, लेखक, वक्ता, धनी, गरीब आदि की मान्यताएँ प्राण भूमिका में होती हैं। मनोमय कोश की स्थिति में पहुँचने पर अपने मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है। लोभी, दम्भी, चोर, उदार, विषयी, संयमी, नास्तिक, आस्तिक, स्वार्थी, परमार्थी, दयालु, निष्ठुर आदि कर्त्तव्य और धर्म की औचित्य-अनौचित्य सम्बन्धी मान्यताएँ जब अपने सम्बन्ध में बनती हों, उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुँचा हुआ है। इससे चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका है, जिसमें पहुँचकर जीव अपने को यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर से, गुणों से, स्वभाव से ऊपर हूँ; मैं ईश्वर का राजकुमार, अविनाशी आत्मा हूँ।
जीभ से अपने को आत्मा कहने वाले असंख्य लोग हैं, उन्हें आत्मज्ञानी नहीं कह सकते। आत्मज्ञानी वह है जो दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भीतर यह अनुभव करता है—‘‘मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। शरीर मेरा वाहन है। प्राण मेरा अस्त्र है। मन मेरा सेवक है। मैं इन सबसे ऊपर, इन सबसे अलग, इन सबका स्वामी आत्मा हूँ। मेरे स्वार्थ इनसे अलग हैं, मेरे लाभ और स्थूल शरीर के लाभों में, स्वार्थों में भारी अन्तर है।’’ इस अन्तर को समझकर जीव अपने लाभ, स्वार्थ, हित और कल्याण के लिए कटिबद्ध होता है, आत्मोन्नति के लिए अग्रसर होता है, तो उसे अपना स्वरूप और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है।
विज्ञानमय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुँचे हुए जीव का दृष्टिकोण सांसारिक जीवों से भिन्न होता है। गीता में योगी का लक्षण बताया गया है कि जब सब जीव सोते हैं, तब योगी जागता है और सब जीव जब जागते हैं, तब योगी सो जाता है। इन आलंकारिक शब्दों में रात को जागने और दिन में सोने का विधान नहीं है, वरन् यह बताया गया है कि जिन चीजों के लिए साधारण लोग बेतरह इच्छुक, प्यासे, लालायित, सतृष्ण और आकांक्षी रहते हैं, योगी का मन इधर से फिर जाता है; क्योंकि वह देखता है कि कामिनी और कञ्चन की माया शरीर को गुदगुदाती है, पर आत्मा को ले बैठती है। इससे क्षणिक सुख के लिए स्थिर आनन्द का नाश करना उचित नहीं है। जिन धन-सन्तान, कुटुम्ब-कबीला, शत्रु-मित्र, हानि-लाभ, आगा-पीछा, निन्दा-स्तुति आदि की समस्याओं में साधारण लोग बेतरह फँसे रहते हैं, ये बातें योगियों के लिए अबोध बच्चों की ‘बालक्रीड़ा’ से अधिक कुछ भी महत्त्व की दिखाई नहीं देतीं; इसलिए वे उनकी ओर से उदास हो जाते हैं। वे इस झमेले को बहुत कम महत्त्व देते हैं। फलस्वरूप यह समस्याएँ उनके लिए अपने आप सुलझ जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं।
जिन कार्यों में, विचारों में कामी लोग, मायाग्रस्त व्यक्ति अत्यन्त मोहग्रस्त होकर चिपके रहते हैं, उनकी ओर से योगी मुँह फेर लेते हैं। इस प्रकार वे वहाँ सोये हुए माने जाते हैं, जहाँ कि अन्य जीव जागते हैं। इसी प्रकार जिन कार्यों की ओर, संयम, त्याग, परमार्थ, आत्मलाभ की ओर सांसारिक जीवों का बिलकुल ध्यान नहीं होता, उनमें योगी दत्तचित्त होकर संलग्न रहते हैं। इस स्थिति के बारे में ही गीता में कहा गया है कि जब जीव सोते हैं, तब योगी जागते हैं।
शरीर यात्रा के लिए प्राय: सभी मनुष्यों को मिलता-जुलता कार्यक्रम रखना पड़ता है, पर योगी और भोगी के जीवन तथा रीति में भारी अन्तर होता है। प्राय: सभी लोग तड़के नित्यकर्म से निवृत होते और भोजन करके काम में लगते हैं। शाम तक जो श्रम करना पड़ता है, उसमें से अधिकांश समय अन्न, वस्त्र और जीवन आश्रितों की व्यवस्था में लग जाता है। शाम को फिर नित्यकर्म, भोजन और रात को सो जाना। इस धुरी पर सबका जीवन घूमता है, परन्तु अन्त:स्थिति में जमीन-आसमान का भेद है। एक मनुष्य अपने शरीर के लिए धन और भोग इकट्ठे करने की योजना सामने रखकर अपने हर विचार और कार्य को करता है, जबकि दूसरा अपने आत्मा को समझकर आत्मकल्याण की नीति पर चलता है। ये विभिन्न दृष्टिकोण ही एक के कामों को पुण्य एवं यज्ञ बना देते हैं और दूसरे के काम पाप एवं बन्धन बन जाते हैं।
आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, आत्मलाभ, आत्मप्राप्ति, आत्मदर्शन, आत्मकल्याण को जीवन लक्ष्य माना गया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होता है जब हमारी अन्त:चेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास-भावना के साथ यह अनुभव करे कि मैं वस्तुत: परब्रह्म परमात्मा की अविच्छिन्न अंश, अविनाशी आत्मा हूँ। इस भावना की पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्मसाक्षात्कार है।
आत्मसाक्षात्कार की चार साधनाएँ नीचे दी जाती हैं—(१) सोऽहं साधना, (२) आत्मानुभूति, (३) स्वर संयम, (४) ग्रन्थिभेद । ये चारों ही विज्ञानमय कोश को प्रबुद्ध करने वाली हैं।
Versions
-

ENGLISHSuper Science of GayatriScan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानScan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 1Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 2Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 3Scan Book Version
-
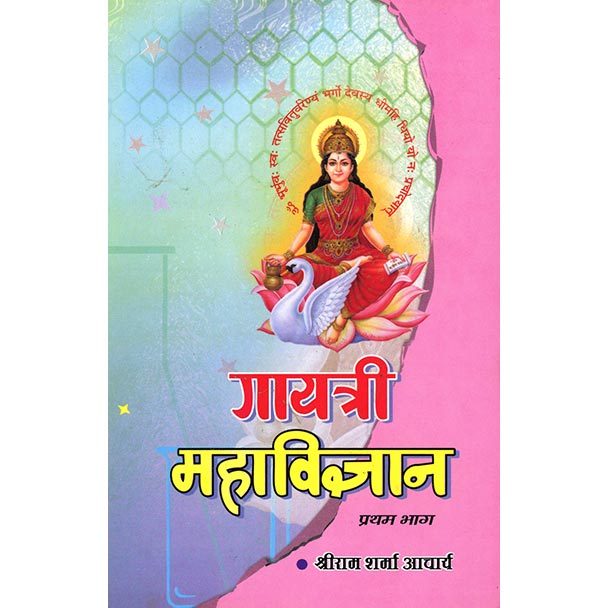
MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग १Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग २Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग ३Scan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानText Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग)Text Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान भाग 2Text Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री महाविज्ञान भाग १
- वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति
- ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव
- गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है
- गायत्री साधना से शक्तिकोशों का उद्भव
- शरीर में गायत्री मंत्र के अक्षर
- गायत्री और ब्रह्म की एकता
- महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान
- त्रिविध दु:खों का निवारण
- गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना
- गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता
- गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण
- जीवन का कायाकल्प
- नारियों को वेद एवं गायत्री का अधिकार
- देवियों की गायत्री साधना
- गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य
- गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत (जनेऊ)
- साधकों के लिये उपवीत आवश्यक है
- गायत्री साधना का उद्देश्य
- निष्काम साधना का तत्त्व ज्ञान
- गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध
- साधना- एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- आत्मशक्ति का अकूत भण्डार :: अनुष्ठान
- सदैव शुभ गायत्री यज्ञ
- महिलाओं के लिये विशेष साधनाएँ
- एक वर्ष की उद्यापन साधना
- गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि
- गायत्री का अर्थ चिन्तन
- साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते
- साधना की सफलता के लक्षण
- सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिये
- गायत्री द्वारा कुण्डलिनी जागरण
- यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बाँटिये
- गायत्री महाविज्ञान भाग ३ भूमिका
- गायत्री के पाँच मुख
- अनन्त आनन्द की साधना
- गायत्री मञ्जरी
- अन्नमय कोश और उसकी साधना
- उपवास - अन्नमय कोश की साधना
- आसन - अन्नमय कोश की साधना
- तत्त्व शुद्धि - अन्नमय कोश की साधना
- तपश्चर्या - अन्नमय कोश की साधना
- मनोमय कोश की साधना
- ध्यान - मनोमय कोश की साधना
- त्राटक - मनोमय कोश की साधना
- जप - मनोमय कोश की साधना
- तन्मात्रा साधना - मनोमय कोश की साधना
- विज्ञानमय कोश की साधना
- सोऽहं साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मानुभूति योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मचिन्तन की साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- स्वर योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- वायु साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- ग्रन्थि-भेद - विज्ञानमय कोश की साधना
- आनन्दमय कोश की साधना
- नाद साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- बिन्दु साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- कला साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- तुरीयावस्था - आनन्दमय कोश की साधना
- पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य
- गायत्री-साधना निष्फल नहीं जाती
- पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य
- गायत्री का तन्त्रोक्त वाम-मार्ग
- गायत्री की गुरु दीक्षा
- आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- मन्त्र दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- अग्नि दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्म दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- कल्याण मन्दिर का प्रवेश द्वार - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्मदीक्षा की दक्षिणा आत्मदान - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- वर्तमानकालीन कठिनाइयाँ - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ

