गायत्री महाविज्ञान 
ब्रह्मदीक्षा की दक्षिणा आत्मदान - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
Read Scan Version
क्रमश: दीक्षा का महत्त्व बढ़ता है, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ता है। जो वस्तु जितनी बढ़िया होती है उसका मूल्य भी उसी अनुपात में होता है। लोहा सस्ता बिकता है, कम पैसे देकर मामूली दुकानदार से लोहे की वस्तु खरीदी जा सकती है। पर यदि सोना या जवाहरात खरीदने हों, तो ऊँची दुकान पर जाना पड़ेगा और अधिक दाम खर्च करना पड़ेगा। ब्रह्मदीक्षा में न विचारशक्ति से काम चलता है और न प्राणशक्ति से। एक आत्मा से दूसरी आत्मा ‘परा’ वाणी द्वारा वार्तालाप करती है। आत्मा की भाषा को परा कहते हैं। वैखरी भाषा को कान सुनते हैं, ‘मध्यमा’ को मन सुनता है, पश्यन्ती हृदय को सुनाई पड़ती है और ‘परा’ वाणी द्वारा दो आत्माओं में सम्भाषण होता है। अन्य वाणियों की बात आत्मा नहीं समझ सकती। जैसे चींटी की समझ में मनुष्य की वाणी नहीं आती और मनुष्य चींटी की वाणी नहीं सुन पाता, उसी प्रकार आत्मा तक व्याख्यान आदि नहीं पहुँचते। उपनिषद् का वचन है कि ‘‘बहुत पढ़ने से व बहुत सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। बलहीनों को भी वह प्राप्त नहीं होती।’’ कारण स्पष्ट है कि यह बातें आत्मा तक पहुँचती ही नहीं, तो वह सुनी कैसे जायेंगी?
कीचड़ में फँसे हुए हाथी को दूसरा हाथी ही निकालता है। पानी में बहते जाने वाले को कोई तैरने वाला ही पार निकालता है। राजा की सहायता करना किसी राजा को ही सम्भव है। एक आत्मा में ब्रह्मज्ञान जाग्रत् करना, उसे ब्राह्मीभूत, ब्रह्मपरायण बनाना केवल उसी के लिए सम्भव है जो स्वयं ब्रह्मतत्त्व में ओत-प्रोत हो रहा हो। जिसमें स्वयं अग्रि होगी, वही दूसरो को प्रकाश और गर्मी दे सकेगा। अन्यथा अग्रि का चित्र कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा।
कई व्यक्ति साधु महात्माओं का वेश बना लेते हैं, पर उनमें ब्रह्मतेज की अग्रि नहीं होती। जिसमें साधुता हो वही महात्मा है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण है, जिसने रागों से मन को बचा लिया है वही वैरागी है, जो स्वाध्याय में, मनन में लीन रहता हो वही मुनि है, जिसने अहंकार को, मोह-ममता को त्याग दिया है, वही सन्यासी है, जो तप में प्रवृत्त हो वही तपस्वी है। कौन क्या है, इसका निर्णय गुण-कर्म से होता है, वेश से नहीं। इसलिए ब्रह्मपरायण होने के लिए कोई वेश बनाने की आवश्यकता नहीं। दूसरों को बिना प्रदर्शन किए, सीधे-सादे तरीके से रहकर जब आत्मकल्याण किया जा सकता है, जो व्यर्थ में लोक दिखावा क्यों किया जाय? सादा वस्त्र, सादा वेश और सादा जीवन में जब महानतम आत्मिक साधना हो सकती है, तो असाधरण वेश तथा अस्थिर कार्यक्रम क्यों अपनाया जाय? पुराने समय अब नहीं रहे, पुरानी परिस्थितियाँ भी अब नहीं हैं; आज की स्थिति में सादा जीवन में ही आत्मिक विकास की सम्भावना अधिक है।
ब्राह्मी दृष्टि का प्राप्त होना ब्रह्मसमाधि है। सर्वत्र सब में ईश्वर का दिखाई देना, अपने अन्दर तेजपुञ्ज की उज्ज्वल झाँकी होना, अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य, दैवी हो जाना यही ब्राह्मी स्थिति है। पूर्व युगों में आकाश तत्त्व की प्रधानता थी। दीर्घ काल तक प्राणों को रोककर ब्रह्माण्ड में एकत्रित कर लेना और शरीर को नि:चेष्ट कर देना समाधि कहलाता था। ध्यान काल में पूर्ण तन्मयता होना और शरीर की सुधि-बुधि भूल जाना उन युगों में ‘समाधि’ कहलाता था। उन युगो में वायु और अग्रि तत्त्वों की प्रधानता थी । आज के युग में जल और पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता होने से ब्राह्मी स्थिति को ही समाधि कहते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवत्गीता के दूसरे अध्याय में इसी ब्रह्मसमाधि की विस्तारपूर्वक शिक्षा दी गयी है। उस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्मसमाधिस्थ ही कहा जायेगा।
अभी भी कई व्यक्ति जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बन्द हो जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ सिद्ध करते हैं। यह बालक्रीड़ा अत्यन्त उपहासास्पद है। वह मन की घबराहट पर काबू पाने की मानसिक साधना का चमत्कार मात्र है। अन्यथा लम्बे-चौड़े गड्ढे में क्या कोई भी आदमी काफी लम्बी अवधि तक सुखपूर्वक रह सकता है? रात भर लोग रुई की रजाई में मुँह बन्द करके सोते रहते हैं, रजाई के भीतर की जरा-सी हवा से रात भर का गुजारा हो जाता है, तो लम्बे चौड़े गड्ढे की हवा आसानी से दस पन्द्रह दिन काम दे सकती है। फिर भूमि में स्वयं भी हवा रहती है। गुफाओं में रहने का अभ्यासी मनुष्य आसानी से जमीन में गड़ने की समाधि का प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे क्रीड़ा-कौतुकों की ओर ध्यान देने की सच्चे ब्रह्मज्ञानी को कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती।
परावाणी द्वारा अन्तरंग प्रेरणा
आत्मा में ब्रह्म तत्त्व का प्रवेश करने में दूसरी आत्मा द्वारा आया हुआ ब्रह्म-संस्कार बड़ा काम करता है। साँप जब किसी को काटता है तो तिल भर जगह में दाँत गाड़ता है और विष भी कुछ रत्ती भर ही डालता है, पर विष धीरे-धीरे सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है, सारी देह विषैली हो जाती है और अन्त में परिणाम मृत्यु होता है। ब्रह्म-दीक्षा भी आध्यात्मिक सर्प-दंशन है। एक का विष दूसरे को चढ़ जाता है। अग्रि की एक चिनगारी सारे ढेर को अग्रिरूप कर देती है। भली प्रकार स्थित किया हुआ दीक्षा संस्कार तेजी से फैलता है और थोड़े ही समय में पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञान की पुस्तक पढ़ते रहने और आध्यात्मिक प्रवचन करते रहने से मनोभूमि तो तैयार होती है, पर बीज बोये बिना अंकुर नहीं उगता और अंकुर को सींचे बिना शीतल छाया और मधुर फल देने वाला वृक्ष नहीं होता। स्वाध्याय और सत्संग के अतिरिक्त आत्मकल्याण के लिए साधना की भी आवश्यकता होती है। साधना की जड़ में सजीव प्राण और सजीव प्रेरणा हो, तो वह अधिक सुगमता और सुविधापूर्वक विकसित होती है।
ब्राह्मी स्थिति का साधक अपने भीतर और बाहर ब्रह्म का पुण्य प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह ब्रह्म की गोदी में किलोल कर रहा है, ब्रह्म के अमृत सिन्धु में आनन्दमग्र हो रहा है। इस दशा में पहुँचकर वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो प्रारब्ध बन चुके हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए वह जीवित रहता है। जब वह हिसाब बराबर हो जाता है तो पूर्ण शान्ति और पूर्ण ब्राह्मी स्थिति में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर उसे भव बन्धन में लौटना नहीं होता। प्रारब्धों को पूरा करने के लिए वह शरीर धारण किये रहता है। सामान्य श्रेणी के मनुष्यों की भाँति सीधा-सादा जीवन बिताता है, तो भी उसकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊँची रहती है। हमारी जानकारी में ऐसे अनेक ऋषि, राजर्षि और महर्षि हैं, जो बाह्यत: बहुत ही साधारण रीति से जीवन बिता रहे हैं, पर उनकी आन्तरिक स्थिति सतयुग आदि के श्रेष्ठ ऋषियों के समान ही महान् है। युग प्रभाव से आज चमत्कारों का युग नही रहा, तो भी आत्मा की उन्नति में कभी कोई युग बाधा नहीं डाल सकता। पूर्वकाल में जैसी महान् आत्मायें होती थीं, आज भी वह सब क्रम यथावत् जारी है। उस समय वे योगी आसानी से पहचान लिये जाते थे, आज उनको पहचानना कठिन है। इस कठिनाई के होते हुए भी आत्मविकास का मार्ग सदा की भाँति अब भी खुला हुआ है।
ब्रह्मदीक्षा के अधिकारी गुरु-शिष्य ही इस महान् सम्बन्ध को स्थापित कर सकते हैं। शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है, गुरु उसके कार्यों का उत्तरदायित्व एवं परिणाम अपने ऊपर लेता है। ईश्वर को आत्मसमर्पण करने की प्रथम भूमिका गुरु को आत्मसमर्पण करना है। शिष्य अपना सब कुछ गुरु को समर्पण करता है। गुरु उस सबको अमानत के तौर पर शिष्य को लौटा देता है और आदेश कर देता है कि इन सब वस्तुओं को गुरु की समझ कर उपयोग करो। इस समर्पण से प्रत्यक्षत: कोई विशेष हेर-फेर नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु अपरिग्रही होने के कारण उस सब ‘समर्पण’ का करेगा भी क्या? दूसरे व्यवस्था एवं व्यावहारिकता की दृष्टि से भी उसका सौंपा हुआ सब कुछ उसी के संरक्षण में ठीक प्रकार रह सकता है, इसलिए ब्राह्यत: इस समर्पण में कुछ विशेष बात प्रतीत नहीं होती, पर आत्मिक दृष्टि से इस ‘आत्मदान’ का मूल्य इतना भारी है कि उसकी तुलना और किसी त्याग या पुण्य से नहीं हो सकती।
जब दो चार रुपया दान करने पर मनुष्य को इतना आत्मसन्तोष और पुण्य प्राप्त होता है, तब शरीर भी दान कर देने से पुण्य और आत्मसन्तोष की अन्तिम मर्यादा समाप्त हो जाती है। आत्मदान से बड़ा और कोई दान इस संसार में किसी प्राणी से सम्भव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी तुलना में इस विश्व ब्रह्माण्ड में और कोई पुण्य फल भी नहीं है। नित्य सवा मन सोने का दान करने वाला कर्ण ‘दानवीर’ के नाम से प्रसिद्ध था, पर उसके पास भी दान के बाद कुछ न कुछ अपना रह जाता था। जिस दानी ने अपना कुछ छोड़ा ही नहीं, उसकी तुलना किसी दानी से नहीं हो सकती।
‘आत्मदान’ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक महान् कार्य है। अपनी सब वस्तुएँ जब वह गुरु की, अन्त में परमात्मा की समझकर उनके आदेशानुसार नौकर की भाँति प्रयोग करता है, तो उसका स्वार्थ, मोह, अहंकार, मान, मद, मत्सर, क्रोध आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। जब अपना कुछ रहा ही नहीं तो ‘मेरा’ क्या? अहंकार किस बात का? जब उपार्जित की हुई वस्तुओं का स्वामी गुरु या परमात्मा ही है तो स्वार्थ कैसा? जब हम नौकर मात्र रह गये तो हानि-लाभ में शोक सन्ताप कैसा? इस प्रकार ‘आत्मदान’ में वस्तुत: ‘अहंकार’ का दान होता है। वस्तुओं के प्रति ‘मेरी’ भावना न रहकर ‘गुरु की’ या ‘परमात्मा की’ भावना हो जाती है। यह ‘भावना परिवर्तन, आत्मपरिवर्तन’ एक असाधारण एवं रहस्यमय प्रक्रिया है। इसके द्वारा साधक सहज ही बन्धनों से खुल जाता है। अहंकार के कारण जो अनेक संस्कार उसके ऊपर लदते थे, वे एक भी ऊपर नहीं लदते। जैसे छोटा बालक अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेता, उसका सब कुछ बोझ माता-पिता पर रहता है, इसी प्रकार आत्मदानी का बोझ भी किसी दूसरी उच्च सत्ता पर चला जाता है।
ब्रह्मदीक्षा का शिष्य गुरु को ‘आत्मदान’ करता है। मन्त्रदीक्षित को ‘गुरु पूजा’ करनी पड़ती है। अग्निदीक्षित को ‘गुरुदक्षिणा’ देनी पड़ती है। ब्रह्मदीक्षित को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। राम को राज्य का अधिकारी मानकर उनकी खड़ाऊ सिंहासन पर रख कर जैसे भरत राज काज चलाते रहे, वैसे ही आत्मदानी अपनी वस्तुओं का समर्पण करके उनके व्यवस्थापक के रूप में स्वयं काम करता रहता है।
कीचड़ में फँसे हुए हाथी को दूसरा हाथी ही निकालता है। पानी में बहते जाने वाले को कोई तैरने वाला ही पार निकालता है। राजा की सहायता करना किसी राजा को ही सम्भव है। एक आत्मा में ब्रह्मज्ञान जाग्रत् करना, उसे ब्राह्मीभूत, ब्रह्मपरायण बनाना केवल उसी के लिए सम्भव है जो स्वयं ब्रह्मतत्त्व में ओत-प्रोत हो रहा हो। जिसमें स्वयं अग्रि होगी, वही दूसरो को प्रकाश और गर्मी दे सकेगा। अन्यथा अग्रि का चित्र कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा।
कई व्यक्ति साधु महात्माओं का वेश बना लेते हैं, पर उनमें ब्रह्मतेज की अग्रि नहीं होती। जिसमें साधुता हो वही महात्मा है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण है, जिसने रागों से मन को बचा लिया है वही वैरागी है, जो स्वाध्याय में, मनन में लीन रहता हो वही मुनि है, जिसने अहंकार को, मोह-ममता को त्याग दिया है, वही सन्यासी है, जो तप में प्रवृत्त हो वही तपस्वी है। कौन क्या है, इसका निर्णय गुण-कर्म से होता है, वेश से नहीं। इसलिए ब्रह्मपरायण होने के लिए कोई वेश बनाने की आवश्यकता नहीं। दूसरों को बिना प्रदर्शन किए, सीधे-सादे तरीके से रहकर जब आत्मकल्याण किया जा सकता है, जो व्यर्थ में लोक दिखावा क्यों किया जाय? सादा वस्त्र, सादा वेश और सादा जीवन में जब महानतम आत्मिक साधना हो सकती है, तो असाधरण वेश तथा अस्थिर कार्यक्रम क्यों अपनाया जाय? पुराने समय अब नहीं रहे, पुरानी परिस्थितियाँ भी अब नहीं हैं; आज की स्थिति में सादा जीवन में ही आत्मिक विकास की सम्भावना अधिक है।
ब्राह्मी दृष्टि का प्राप्त होना ब्रह्मसमाधि है। सर्वत्र सब में ईश्वर का दिखाई देना, अपने अन्दर तेजपुञ्ज की उज्ज्वल झाँकी होना, अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य, दैवी हो जाना यही ब्राह्मी स्थिति है। पूर्व युगों में आकाश तत्त्व की प्रधानता थी। दीर्घ काल तक प्राणों को रोककर ब्रह्माण्ड में एकत्रित कर लेना और शरीर को नि:चेष्ट कर देना समाधि कहलाता था। ध्यान काल में पूर्ण तन्मयता होना और शरीर की सुधि-बुधि भूल जाना उन युगों में ‘समाधि’ कहलाता था। उन युगो में वायु और अग्रि तत्त्वों की प्रधानता थी । आज के युग में जल और पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता होने से ब्राह्मी स्थिति को ही समाधि कहते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवत्गीता के दूसरे अध्याय में इसी ब्रह्मसमाधि की विस्तारपूर्वक शिक्षा दी गयी है। उस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्मसमाधिस्थ ही कहा जायेगा।
अभी भी कई व्यक्ति जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बन्द हो जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ सिद्ध करते हैं। यह बालक्रीड़ा अत्यन्त उपहासास्पद है। वह मन की घबराहट पर काबू पाने की मानसिक साधना का चमत्कार मात्र है। अन्यथा लम्बे-चौड़े गड्ढे में क्या कोई भी आदमी काफी लम्बी अवधि तक सुखपूर्वक रह सकता है? रात भर लोग रुई की रजाई में मुँह बन्द करके सोते रहते हैं, रजाई के भीतर की जरा-सी हवा से रात भर का गुजारा हो जाता है, तो लम्बे चौड़े गड्ढे की हवा आसानी से दस पन्द्रह दिन काम दे सकती है। फिर भूमि में स्वयं भी हवा रहती है। गुफाओं में रहने का अभ्यासी मनुष्य आसानी से जमीन में गड़ने की समाधि का प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे क्रीड़ा-कौतुकों की ओर ध्यान देने की सच्चे ब्रह्मज्ञानी को कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती।
परावाणी द्वारा अन्तरंग प्रेरणा
आत्मा में ब्रह्म तत्त्व का प्रवेश करने में दूसरी आत्मा द्वारा आया हुआ ब्रह्म-संस्कार बड़ा काम करता है। साँप जब किसी को काटता है तो तिल भर जगह में दाँत गाड़ता है और विष भी कुछ रत्ती भर ही डालता है, पर विष धीरे-धीरे सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है, सारी देह विषैली हो जाती है और अन्त में परिणाम मृत्यु होता है। ब्रह्म-दीक्षा भी आध्यात्मिक सर्प-दंशन है। एक का विष दूसरे को चढ़ जाता है। अग्रि की एक चिनगारी सारे ढेर को अग्रिरूप कर देती है। भली प्रकार स्थित किया हुआ दीक्षा संस्कार तेजी से फैलता है और थोड़े ही समय में पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञान की पुस्तक पढ़ते रहने और आध्यात्मिक प्रवचन करते रहने से मनोभूमि तो तैयार होती है, पर बीज बोये बिना अंकुर नहीं उगता और अंकुर को सींचे बिना शीतल छाया और मधुर फल देने वाला वृक्ष नहीं होता। स्वाध्याय और सत्संग के अतिरिक्त आत्मकल्याण के लिए साधना की भी आवश्यकता होती है। साधना की जड़ में सजीव प्राण और सजीव प्रेरणा हो, तो वह अधिक सुगमता और सुविधापूर्वक विकसित होती है।
ब्राह्मी स्थिति का साधक अपने भीतर और बाहर ब्रह्म का पुण्य प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह ब्रह्म की गोदी में किलोल कर रहा है, ब्रह्म के अमृत सिन्धु में आनन्दमग्र हो रहा है। इस दशा में पहुँचकर वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो प्रारब्ध बन चुके हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए वह जीवित रहता है। जब वह हिसाब बराबर हो जाता है तो पूर्ण शान्ति और पूर्ण ब्राह्मी स्थिति में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर उसे भव बन्धन में लौटना नहीं होता। प्रारब्धों को पूरा करने के लिए वह शरीर धारण किये रहता है। सामान्य श्रेणी के मनुष्यों की भाँति सीधा-सादा जीवन बिताता है, तो भी उसकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊँची रहती है। हमारी जानकारी में ऐसे अनेक ऋषि, राजर्षि और महर्षि हैं, जो बाह्यत: बहुत ही साधारण रीति से जीवन बिता रहे हैं, पर उनकी आन्तरिक स्थिति सतयुग आदि के श्रेष्ठ ऋषियों के समान ही महान् है। युग प्रभाव से आज चमत्कारों का युग नही रहा, तो भी आत्मा की उन्नति में कभी कोई युग बाधा नहीं डाल सकता। पूर्वकाल में जैसी महान् आत्मायें होती थीं, आज भी वह सब क्रम यथावत् जारी है। उस समय वे योगी आसानी से पहचान लिये जाते थे, आज उनको पहचानना कठिन है। इस कठिनाई के होते हुए भी आत्मविकास का मार्ग सदा की भाँति अब भी खुला हुआ है।
ब्रह्मदीक्षा के अधिकारी गुरु-शिष्य ही इस महान् सम्बन्ध को स्थापित कर सकते हैं। शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है, गुरु उसके कार्यों का उत्तरदायित्व एवं परिणाम अपने ऊपर लेता है। ईश्वर को आत्मसमर्पण करने की प्रथम भूमिका गुरु को आत्मसमर्पण करना है। शिष्य अपना सब कुछ गुरु को समर्पण करता है। गुरु उस सबको अमानत के तौर पर शिष्य को लौटा देता है और आदेश कर देता है कि इन सब वस्तुओं को गुरु की समझ कर उपयोग करो। इस समर्पण से प्रत्यक्षत: कोई विशेष हेर-फेर नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु अपरिग्रही होने के कारण उस सब ‘समर्पण’ का करेगा भी क्या? दूसरे व्यवस्था एवं व्यावहारिकता की दृष्टि से भी उसका सौंपा हुआ सब कुछ उसी के संरक्षण में ठीक प्रकार रह सकता है, इसलिए ब्राह्यत: इस समर्पण में कुछ विशेष बात प्रतीत नहीं होती, पर आत्मिक दृष्टि से इस ‘आत्मदान’ का मूल्य इतना भारी है कि उसकी तुलना और किसी त्याग या पुण्य से नहीं हो सकती।
जब दो चार रुपया दान करने पर मनुष्य को इतना आत्मसन्तोष और पुण्य प्राप्त होता है, तब शरीर भी दान कर देने से पुण्य और आत्मसन्तोष की अन्तिम मर्यादा समाप्त हो जाती है। आत्मदान से बड़ा और कोई दान इस संसार में किसी प्राणी से सम्भव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी तुलना में इस विश्व ब्रह्माण्ड में और कोई पुण्य फल भी नहीं है। नित्य सवा मन सोने का दान करने वाला कर्ण ‘दानवीर’ के नाम से प्रसिद्ध था, पर उसके पास भी दान के बाद कुछ न कुछ अपना रह जाता था। जिस दानी ने अपना कुछ छोड़ा ही नहीं, उसकी तुलना किसी दानी से नहीं हो सकती।
‘आत्मदान’ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक महान् कार्य है। अपनी सब वस्तुएँ जब वह गुरु की, अन्त में परमात्मा की समझकर उनके आदेशानुसार नौकर की भाँति प्रयोग करता है, तो उसका स्वार्थ, मोह, अहंकार, मान, मद, मत्सर, क्रोध आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। जब अपना कुछ रहा ही नहीं तो ‘मेरा’ क्या? अहंकार किस बात का? जब उपार्जित की हुई वस्तुओं का स्वामी गुरु या परमात्मा ही है तो स्वार्थ कैसा? जब हम नौकर मात्र रह गये तो हानि-लाभ में शोक सन्ताप कैसा? इस प्रकार ‘आत्मदान’ में वस्तुत: ‘अहंकार’ का दान होता है। वस्तुओं के प्रति ‘मेरी’ भावना न रहकर ‘गुरु की’ या ‘परमात्मा की’ भावना हो जाती है। यह ‘भावना परिवर्तन, आत्मपरिवर्तन’ एक असाधारण एवं रहस्यमय प्रक्रिया है। इसके द्वारा साधक सहज ही बन्धनों से खुल जाता है। अहंकार के कारण जो अनेक संस्कार उसके ऊपर लदते थे, वे एक भी ऊपर नहीं लदते। जैसे छोटा बालक अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेता, उसका सब कुछ बोझ माता-पिता पर रहता है, इसी प्रकार आत्मदानी का बोझ भी किसी दूसरी उच्च सत्ता पर चला जाता है।
ब्रह्मदीक्षा का शिष्य गुरु को ‘आत्मदान’ करता है। मन्त्रदीक्षित को ‘गुरु पूजा’ करनी पड़ती है। अग्निदीक्षित को ‘गुरुदक्षिणा’ देनी पड़ती है। ब्रह्मदीक्षित को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। राम को राज्य का अधिकारी मानकर उनकी खड़ाऊ सिंहासन पर रख कर जैसे भरत राज काज चलाते रहे, वैसे ही आत्मदानी अपनी वस्तुओं का समर्पण करके उनके व्यवस्थापक के रूप में स्वयं काम करता रहता है।
Versions
-

ENGLISHSuper Science of GayatriScan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानScan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 1Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 2Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 3Scan Book Version
-
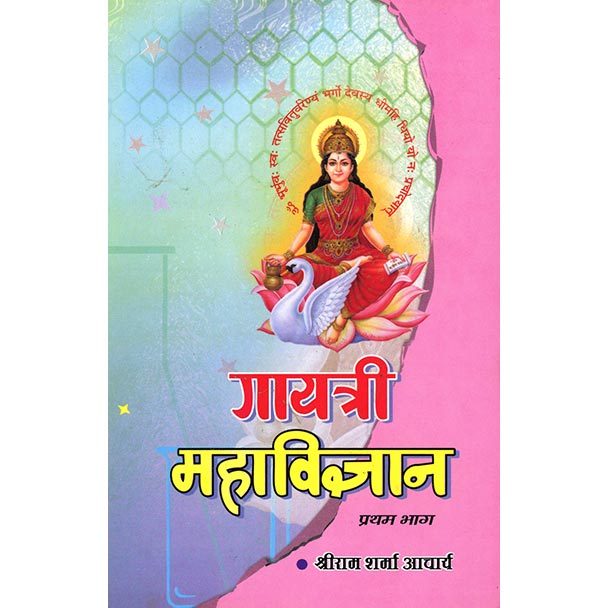
MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग १Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग २Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग ३Scan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानText Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग)Text Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान भाग 2Text Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री महाविज्ञान भाग १
- वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति
- ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव
- गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है
- गायत्री साधना से शक्तिकोशों का उद्भव
- शरीर में गायत्री मंत्र के अक्षर
- गायत्री और ब्रह्म की एकता
- महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान
- त्रिविध दु:खों का निवारण
- गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना
- गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता
- गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण
- जीवन का कायाकल्प
- नारियों को वेद एवं गायत्री का अधिकार
- देवियों की गायत्री साधना
- गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य
- गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत (जनेऊ)
- साधकों के लिये उपवीत आवश्यक है
- गायत्री साधना का उद्देश्य
- निष्काम साधना का तत्त्व ज्ञान
- गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध
- साधना- एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए
- पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ
- आत्मशक्ति का अकूत भण्डार :: अनुष्ठान
- सदैव शुभ गायत्री यज्ञ
- महिलाओं के लिये विशेष साधनाएँ
- एक वर्ष की उद्यापन साधना
- गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि
- गायत्री का अर्थ चिन्तन
- साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते
- साधना की सफलता के लक्षण
- सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिये
- गायत्री द्वारा कुण्डलिनी जागरण
- यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बाँटिये
- गायत्री महाविज्ञान भाग ३ भूमिका
- गायत्री के पाँच मुख
- अनन्त आनन्द की साधना
- गायत्री मञ्जरी
- अन्नमय कोश और उसकी साधना
- उपवास - अन्नमय कोश की साधना
- आसन - अन्नमय कोश की साधना
- तत्त्व शुद्धि - अन्नमय कोश की साधना
- तपश्चर्या - अन्नमय कोश की साधना
- मनोमय कोश की साधना
- ध्यान - मनोमय कोश की साधना
- त्राटक - मनोमय कोश की साधना
- जप - मनोमय कोश की साधना
- तन्मात्रा साधना - मनोमय कोश की साधना
- विज्ञानमय कोश की साधना
- सोऽहं साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मानुभूति योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- आत्मचिन्तन की साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- स्वर योग - विज्ञानमय कोश की साधना
- वायु साधना - विज्ञानमय कोश की साधना
- ग्रन्थि-भेद - विज्ञानमय कोश की साधना
- आनन्दमय कोश की साधना
- नाद साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- बिन्दु साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- कला साधना - आनन्दमय कोश की साधना
- तुरीयावस्था - आनन्दमय कोश की साधना
- पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य
- गायत्री-साधना निष्फल नहीं जाती
- पञ्चमुखी साधना का उद्देश्य
- गायत्री का तन्त्रोक्त वाम-मार्ग
- गायत्री की गुरु दीक्षा
- आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- मन्त्र दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- अग्नि दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्म दीक्षा - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- कल्याण मन्दिर का प्रवेश द्वार - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- ब्रह्मदीक्षा की दक्षिणा आत्मदान - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ
- वर्तमानकालीन कठिनाइयाँ - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ

