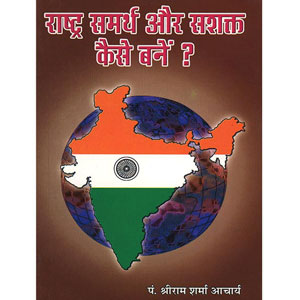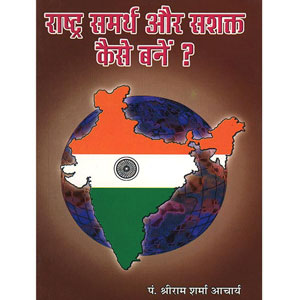राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बनें? 
आत्म-निरीक्षण की घड़ी आ पहुंची
Read Scan Versionसंसार में उन वस्तुओं का सम्मान होता है, जो उपयोगी होती हैं। अपनी उपयोगिता के बल पर ही कोई वस्तु लोकप्रिय, चिरस्थायी और सुविकसित रह सकती है। जिसकी जितनी उपयोगिता घटती है, उसकी उतनी उपेक्षा होती है और धीरे-धीरे जब वह घटोत्तरी बहुत अधिक हो जाती है, तो उस अनुपयोगी वस्तु से लोग घृणा करने लगते हैं और उसके नाश की तैयारी होने लगती है।
कमाऊ युवा पुरुष जो परिवार संचालन के लिये उपयोगी सिद्ध होते हैं—घर भर का सम्मान पाते हैं। उनके मरने पर घर भर में कुहराम मच जाता है, पर वही व्यक्ति जब वृद्ध होकर अपनी उपयोगिता खोकर घर के लोगों के लिये भार बन जाता है, तब उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, उसके मरने पर किसी को गहरा रंज नहीं होता, सच तो यह है कि बहुत दिन पहले से ही उसके मरने की प्रतीक्षा की जाने लगती है। युवा वृद्ध ही क्यों? संसार की हर वस्तु के बारे में यही नियम काम करता है। उपयोगिता के कारण ही कोई वस्तु लोकप्रिय होती और आदर पाती है। लोग हर चीज को लाभ-हानि की कसौटी पर कसते हैं। खरी का सम्मान और खोटी का तिरस्कार, यह प्रथा चिरकाल से चली आ रही है।
धर्म के बारे में भी यही बात है। किसी समय यह देश धर्म-प्राण था, हर व्यक्ति धर्म के लिये अपनी जान देने और उसके लिये सब कुछ निछावर करने को तैयार रहता था, पर अब उसकी सर्वत्र उपेक्षा होती है। नई पीढ़ी के बच्चे उसका उपहास करते हैं। तार्किक लोग उसे व्यर्थ मानते हैं और उस झंझट से बचने की कोशिश करते हैं। इससे आगे बढ़े हुये अधिक उत्साही लोग उसे हानिकारक बताते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। कम्युनिस्ट अथवा वैसी ही विचारधारा के लोगों का धर्म के प्रति घृणा एवं विरोध का भाव प्रसिद्ध ही है।
ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? इस प्रश्न पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। किसी समय के धर्म-प्राण देश में विचारशील लोग उसका तिरस्कार एवं उपहास करें, इसका कुछ तो कारण होना ही चाहिये। यों रूढ़िवादी लोग अन्यमनस्क अभिरुचि के साथ पुरानी लकीर को पीटते रहते हैं, पर उनमें भी श्रद्धा दिखाई नहीं पड़ती। कोई स्वल्प व्यय में पापों के नाम और मनोरथों की पूर्ति के लिये, कोई दिखावे और प्रशंसा के लिये, कोई परंपरा की लकीर पीटने के लिये धर्म की चिह्न पूजा तो कर लेते हैं, पर ऐसी श्रद्धा किन्हीं विरलों में ही होगी जिन्हें धर्म-प्राण कहा जा सके।
रूढ़िवादी लोग किसी प्रकार धर्म की चिह्न-पूजा करते रहे, इतने मात्र से कुछ काम नहीं चल सकता। इतने भर से धर्म की प्रतिष्ठा एवं सामर्थ्य अक्षुण्य नहीं रह सकती। विचारशील, बुद्धिवादी सुशिक्षित एवं समझदार लोग ही किसी समाज की रीढ़ कहलाते हैं। वे जैसा सोचते और जैसा करते हैं, देर-सवेर में सामान्य एवं स्तर के लोगों को भी उनका अनुकरण करना होता है। यदि आज विचारशील लोगों में से धार्मिकता घट रही है, तो कल सामान्य लोगों में से भी घटेगी ही।
नेतृत्व सदा बुद्धिजीवी लोगों के हाथों में रहा है। हजार पिछड़े हुए लोगों की अपेक्षा एक विचारशील का महत्त्व अधिक है। आज हम सुशिक्षित वर्ग के प्रति उदासीनता या उपेक्षा भाव धारण किये देखते हैं। नई पीढ़ी के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक शिखा-सूत्र जैसे धर्म-चिह्नों को धारण करने में अपनी हेठी मानते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों से दूर रहते हैं। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कल इन्हीं लोगों के हाथ में नेतृत्व जाने वाला है। देहातों में यहां-वहां जो धर्म की चिह्न-पूजा आज दिखाई पड़ती है, वह भी वृद्धों के जीवन काल तक चल सकती है। सुशिक्षित एवं विचारशील लोग उसे न अपनावें तो अगले दिनों धर्म की स्थिति दयनीय हुए बिना न रहेगी।
कलियुग आ गया, पाश्चात्य सभ्यता ने नाश कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा बुरी है, जमाना अधार्मिक हो गया, आदि बातें कहकर धर्म के प्रति बढ़ती हुई अश्रद्धा का समाधान नहीं हो सकता। इसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा कि ऐसा परिवर्तन भारत जैसे धर्म प्राण देश में और विशेषतया हिंदुओं में ही क्या हुआ? इस देश में मुसलमान और ईसाई भी रहते हैं। उनके धर्म दर्शन से हिंदू-धर्म दर्शन किसी प्रकार घटिया नहीं, हमारे आदर्श बहुत ऊंचे और सच्चे हैं, ऐसी दशा में हमारी धर्म भावना औरों से अधिक सुदृढ़ होनी चाहिये थी। पर देखा यह जाता है कि अन्य धर्मावलंबी अपने धर्मों पर जितनी श्रद्धा करते हैं, उतनी हम नहीं।
अधिकांश मुसलमान पुरुषों और स्त्रियों का उनके जीवनयापन का ढंग, पहनाव, उढ़ाव, खान-पान, वेश-विन्यास, भाषा, भावना उनके धार्मिक विश्वासों के अनुरूप मिलेगा। ईसाइयों में उनकी धार्मिक श्रद्धा कितना बढ़ी-चढ़ी है। इसका अनुमान उन्हें भारत के अन्य प्रदेश में रहने वाले पिछड़े लोगों एवं हरिजनों के बीच रहते हुए—अभावों और असुविधाओं से भरा जीवन व्यतीत करते हुए देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। जिन पाश्चात्य देशों ने अपना ईसाई धर्म यहां भेजा है उन्होंने उसके लिए पिछले दिनों अरबों रुपया और हजारों लाखों पादरियों के व्यक्तित्व संपन्न जीवन भी दिये हैं। सिखों में अपने धर्म के प्रति भावना है। नवयुवक सिखों को दाढ़ी, केश रखाते, अपने धर्म चिह्न धारण किये देखते हैं, तो उसकी निष्ठा का सहज ही पता लग जाता है।
संसार में अन्य धर्म तेजी से बढ़ रहे हैं। ईसाई धर्म के जन्म को दो हजार वर्ष हुए हैं। उसका व्यवस्थित रूप ईसा के 300 वर्षों बाद सेंटपाल के प्रयत्नों से बन पाया था। इस प्रकार उसे 1700 वर्ष ही होते हैं। इतने स्वल्प समय में उस धर्म ने संसार की लगभग आधी आबादी को अपने विचारों से दीक्षित कर दिया है। संसार में कुल 6 अरब लोग रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व की सूचना के अनुसार ईसाइयों की जनगणना 2 अरब थी। अब तक वह सवाई ड्योढ़ी जरूर हो गई होगी। इस प्रकार लगभग आधी दुनिया ईसाई धर्म में दीक्षित हो गई और उसमें कुछ सत्रह सौ वर्ष लगे।
दूसरे नंबर पर मुसलमान धर्म आता है। उनकी संख्या भी 95 करोड़ से ऊपर है। मध्यकाल में जोर-जबरदस्ती का प्रयोग भली ही रहा हो, पर कोई बात इसी से फलने-फूलने नहीं लग सकती। उसकी कुछ विशेषता भी होनी चाहिए। मुसलमानों के पास ईसाइयों जितने साधन-सुविधा नहीं हैं, फिर भी उनकी निष्ठा ने आश्चर्यजनक विस्तार कर लिया। कुल 1137 वर्षों में 95 करोड़ व्यक्तियों का मुसलमान धर्म में दीक्षित हो जाना इस बात का द्योतक है कि—साधन न भी हों, तो भी निष्ठा के बल पर कोई धर्म संसारव्यापी बन सकता है। अरब में पैदा होकर इस्लाम धर्म अफ्रीका, एशिया, योरोप के छोटे-बड़े प्रायः सभी देशों में काफी गहराई तक अपनी जड़े जमाने में समर्थ हुआ है।
कम्युनिज्म और ईसाइयत से करारी टक्कर लेते हुए भी बौद्धधर्म अभी भी 50 करोड़ से अधिक लोगों का धर्म है। भगवान् बुद्ध को 2500 वर्ष हुए हैं। उनके धर्म का विस्तार महाराज अशोक ने किया। इस प्रकार बौद्धधर्म की प्रसार प्रक्रिया को 21-23 सौ से अधिक वर्ष नहीं हुए। इतने दिनों में इसका विस्तार भी काफी हुआ। आज उनमें भी हिंदुओं जैसे दोष आ जाने से सितारा ढल रहा है। फिर भी हिंदुओं की अपेक्षा वे अभी भी अधिक संख्या में हैं।
उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार भारत में हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या 45 करोड़ है। समस्त संसार में जहां-तहां बिखरे हुए हिंदू एक करोड़ के करीब हैं। इस प्रकार यह संख्या कुल मिलाकर 46 करोड़ हो जाती है। हमारे धर्म का प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि में ही हुआ था। 10 लाख वर्षों से यह समस्त संसार में व्याप्त रहा। अभी संसार भर में हिंदू सभ्यता के जो चिह्न उन देशों के पुरातत्त्व विभागों को मिले हैं, उनसे प्रतीत होता है कि किसी समय इस धरती के कोने-कोने में हिंदू संस्कृति फैली हुई थी। महाभारत काल तक का इतिहास यह बताता है कि, संसार में जितनी भी जनसंख्या थी, वह सभी हिंदू धर्म से दीक्षित थी, देश, काल भाषा आदि के भेदों के कारण वहां हिंदू धर्म का बाह्य स्वरूप थोड़ा-थोड़ा भिन्न था, फिर भी भावनात्मक दृष्टि से समस्त विश्व में हिंदू मान्यताएं ही व्याप्त थीं। संसार भर के विचारशील लोगों ने उसकी महत्ता एवं उपयोगिता को एक स्वर से स्वीकार किया था।
पिछले डेढ़-दो हजार वर्षों में यह आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे हो गया, यह विचारणीय है। बौद्ध, ईसाई, मुसलमान तीनों मिलाकर चार अरब से अधिक हो जाते हैं। उनकी संख्या संसार की आबादी की दो तिहाई है। इसकी तुलना में हिंदू धर्म को देखिये, वह संसार भर से सिकुड़ता हुआ केवल भारत में शेष रह गया है। विदेशों में जो हिंदू हैं, उनमें से अधिकांश भारतवंशीय हैं। क्या अन्य देशों के नागरिक हिंदू धर्म मानते हैं? तो इस संबंध में नकारात्मक ही उत्तर मिलेगा। वंश परंपरागत माध्यम से जो भारतवासी हिंदू बने हुए हैं, उनमें से भी विचारशील लोग जब उपेक्षा, घृणा, तिरस्कार, उपहास और अविश्वास के भाव उसके प्रति रखेंगे तो यही कहा जा सकता है कि एक-दो पीढ़ियों के बाद उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा।
झूठे आत्मसंतोष के लिए हम कलियुग आ गया, धर्म चला गया, पाश्चात्य शिक्षा आ गई आदि बातें कहकर अपने को भुलावे में डाल सकते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। कलियुग हिंदुओं पर ही थोड़े आया है। उसे संसार भर में आना चाहिए था और धर्म के प्रति व्यापक उपेक्षा एवं घृणा भाव बढ़ाना चाहिए था, पर ऐसा न होकर उलटा ही हुआ है। ईसाई धर्म समस्त संसार के हर देश में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए अरबों रुपया खर्च करता है और लाखों सुशिक्षित व्यक्ति धर्म प्रसार में लगे हैं। यदि धर्म के प्रति अश्रद्धा या उपेक्षा होती तो इतनी बड़ी संख्या में धन-जन की व्यवस्था कैसे हुई होती? पाश्चात्य शिक्षा भारत में तो अधकचरी ही है, पर जहां से पैदा हुई और पनपी है, वहां भी तो धर्म की प्रौढ़ता विद्यमान है।
कारण दूसरा ही है, जिस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और वह है अपनी उपयोगिता खोते जाना। हिंदू-धर्म निस्संदेह अपनी उपयोगिता खोता चला जा रहा है। उसमें रहने वाला व्यक्ति जब अन्य धर्मावलंबियों से अपनी तुलना करता है तो उसकी विवेक बुद्धि सहज ही बता देती है कि वह किस समाज में रहता है? वह दूसरों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है। दर्शन उसका कितना ही ऊंचा क्यों न हो, आदर्श उसके कितने ही महान् क्यों न हों, पर व्यवहार का जहां तक संबंध है, वह ऐसा है कि अनुपयुक्त एवं असुविधाजनक ही कहा जा सकता है। दर्शन ऊंचा और व्यवहार नीचा हो तो उसे दंभ ही कहा जा सकता है।
आवश्यकता इस बात की है कि हम गहरा आत्म-निरीक्षण करें और जिन बीमारियों ने समाज शरीर को गलाना शुरू कर दिया है, उसे उपयुक्त चिकित्सा द्वारा निरोग बनाने का प्रयत्न करें। हिंदू-धर्म निश्चित रूप से महान् है, पर वह महानता वेद-पुराणों तक सीमित न रहकर हमारे सामाजिक जीवन में भी व्यवहृत होती हुई दृष्टिगोचर होनी चाहिए। स्थिति चिंताजनक है। दूसरे उसे स्वीकार करें, यह तो प्रश्न पीछे का है। पहली समस्या तो अपनों की उपेक्षा की हल करनी है। यदि यह हल न हुई तो समझना चाहिए—भविष्य अंधकारपूर्ण ही सामने आयेगा।
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- प्रजातंत्र की सफलता के लिए हम यह करें
- हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते?
- लोकमानस के प्रति शासनतंत्र का उत्तरदायित्व
- अनौचित्य के विरुद्ध समर्थ नैतिक क्रांति की आवश्यकता
- प्रगतिशीलता पर ही राष्ट्र का भविष्य निर्भर है
- आत्म-निरीक्षण की घड़ी आ पहुंची
- प्रगति के लिये नागरिक चेतना आवश्यक
- हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रहें
- राष्ट्रीय चरित्र को सुविकसित किया जाए
- हमारी आत्मा मर ही जायेगी क्या?
- प्रगति की दिशा में सही प्रयत्न
- राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में आपका योगदान
- जीवन का उजाला पक्षी भी प्रकाश में आए
- अंग्रेजी की अनिवार्यता हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध है
- छूत-अछूत का भेद क्यों
- अश्लीलता के अजगर से देश को बचाइए
- ग्रामोत्थान—राष्ट्र की आत्मा का उत्थान
- यह सर्वव्यापी भ्रष्टाचार रोका जाए
- खाद्यों में मिलावट की समस्या
- हम विदेशी सहायता के आश्रित
- हम शस्त्रों के लिए किसी के मोहताज न रहें
- बढ़ता मूल्य और गिरता स्तर कैसे रुके?
- व्यक्तिगत प्रगति और सामूहिक समृद्धि के लिए सामूहिकता अनिवार्य
- कृपया जनसंख्या और न बढ़ाइये
- मालिकों को जगाओ—प्रजातंत्र बचाओ
- प्रजा अपने कर्तव्यों से विमुख न हो
- चुनाव की पद्धति बदली जाए
- इतिहास की पुनरावृत्ति