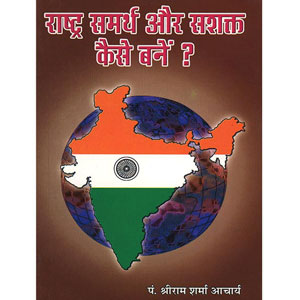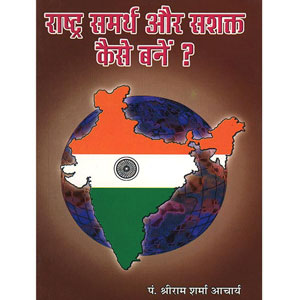राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बनें? 
हमारी आत्मा मर ही जायेगी क्या?
Read Scan Versionविशाल भारत के प्राचीन गौरव की ओर दृष्टिपात करते हैं और अपने पुरखों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि, हमें अपने पूर्व-पुरुषों के ज्ञान और आत्माभिमान का एक छोटा-सा टुकड़ा भी प्राप्त नहीं है। जगद्गुरु की उपाधि से विभूषित होने वाले भारतवर्ष को अब छोटे-छोटे देश भी उंगली दिखाते, हंसते, रौब जमाते हैं। यह सब देखकर हृदय में बड़ी तीव्र बेचैनी उठती है। ऋषियों की शक्ति उनके ज्ञान और गुरुत्व का ध्यान आता है, तो जी करता है कि किसी कोने में बैठकर अपने सारे आंसुओं से धोकर मन का बोझ हल्का कर लें। इस युग में पतन का जो दौर चल रहा है, अब उसे पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ ही समझना चाहिए। इसके आगे तो सर्वनाश के ही लक्षण प्रतीत होते हैं।
राष्ट्र की संपूर्ण विभूति, जिसके कारण यह परम समृद्ध, शक्तिशाली और तत्ववेत्ता था, उसका नाम है—धर्म। यह ‘‘धर्म’’ हमारे पूजा, पाठ तथा प्रथा-परंपराओं की मान्यताओं तक ही सीमित नहीं, वरन् वह मनुष्य जीवन से संबंधित संपूर्ण उत्कृष्टता का आधार है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों, गतिविधियों, दार्शनिकताओं, आचार-विचार, खान-पान, रहन-सहन, नैतिकता आदि का उसमें समावेश है। वह जीवन से संबंधित किसी भी प्रश्न को छोड़ता नहीं, इसलिए धर्म उतना ही विशाल है जितना कि यह विराट जगत। उसे संकीर्णताओं में नहीं बांधा जा सकता। धर्म किसी व्यक्ति का नहीं, उसका कोई नाम भी नहीं, वस्तुतः सनातन सत्य ही धर्म है। उन नियमों की व्यवस्था इतनी प्रायोगिक है कि उसमें प्राणिमात्र का हित समाया हुआ है।
जब तक यह धर्म हमारे जीवन का प्रमुख अंग बना रहा तब तक इस देश में किसी तरह की शिथिलता या दुर्व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई। किंतु नियमों की कठोरता में जब मनमानी बरती जाने लगी और उसमें संकीर्णताओं का समावेश होने लगा तो धर्म से प्राप्त होने वाले गौरव का भी लोप होता चला गया और यह देश एक-एक करके संपूर्ण क्षेत्रों में हारता चला गया।
यों कहने को तो धर्म की शाखा-प्रशाखाएं आज भी किसी तरह कम नहीं हैं। चारों ओर धार्मिक गतिविधियां फैली दिखाई देती हैं। धार्मिक ट्रस्ट, देवालय, धर्म सभायें, योग-मंदिर, सत्संग कुटीर आदि न जाने कितनी संस्थायें, संत और पुजारी धर्म को उन्नत किये रहने का दावा करते हैं, किंतु इन संपूर्ण प्रवृत्तियों के मूल में जाकर देखें तो उसमें भी स्वार्थ, मान, दंभ, पाप और संकीर्णता की भावनायें ही अंतर्हित है। यह देखकर लोगों को धर्म से घृणा होनी ही थी, वही हुआ भी। मनुष्य जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाला धर्म मनोरंजन, स्वार्थ पूर्ति और छल का साधन मात्र बनकर रह गया।
धर्म के संबंध में बड़ी विभिन्नता देखने में आती है। अनेक लोग धर्माचरण करना इसलिए जरूरी समझते हैं कि उसने एक सामाजिक रीति-रिवाज का सा रूप ग्रहण कर लिया है। इससे चतुर लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि में और भी सफलता मिलती है, फलस्वरूप धर्म की यथार्थ भावनाओं में, तप, त्याग और जीवन निर्माण के सदुद्देश्यों में गिरावट ही होती जा रही है।
यह हमारे धार्मिक पतन का एक कारण अपने ही देश और जाति में पाई जाने वाली संकीर्णता है। जब किसी जाति के जीवन में कलुषता बढ़ जाती है, तो उसका सारा आंतरिक ढांचा ही लड़खड़ा जाता है। पाप और पाखंड का समावेश इतना अधिक हुआ कि आध्यात्मिक सद्गुणों का लगभग बहिष्कार-सा कर दिया गया। लोग हल्के-फुल्के कर्मकांड पूरे करने मात्र से स्वर्ग मुक्ति की उपलब्धि सोचने लगे और आत्म-संयम जैसे कष्टसाध्य कार्य से मुंह मोड़ लिया गया। दुर्गुणों के बढ़ने से दुर्व्यवहार बढ़ा और सब तरफ ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट, कलह, निर्धनता, पाशविकता का ही बोलबाला बढ़ता गया। यह स्थिति अब उस स्थान पर पहुंच गई है, जहां रुककर हमें यह सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि—‘हमारी आत्मा मर ही जायेगी क्या?’ क्या भारतवर्ष अपने अतुलनीय प्राचीन गौरव को फिर न पा सकेगा? पड़ौसी संसार के लोगों को समुन्नत होते देखकर यह दर्द और भी बढ़ता है और एक तेज हुंकार के साथ राष्ट्र की सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को बदल डालने को जी चाहता है। राष्ट्र की अंतरात्मा पूर्व धरोहर पाने को एक प्रकार से अकुला ही रही है।
हमें यह मानकर चलना होगा कि रक्षा करने पर भी जो न तो सुख की वृद्धि करता है और न आपत्तियों से बचाव करता है, वह धर्म नहीं है। फिर उसमें अपना कितना ही तात्कालिक हित क्यों न दिखाई पड़ता हो। यदि हम वास्तविक धर्म की उपासना करते होते तो आज पतित, पराधीन, क्षुधार्थ, बीमार, बेकार और तरह-तरह से दीन-हीन न होते। धर्म के साधक की यह दुर्गति न होती, जो अब भुगतनी पड़ रही है। अपनी उन्नति, अपना विकास और वैभव की प्राप्ति—अब इस भूल को सुधारने से ही मिल सकती है। धर्म की शरण में जाने से सब प्रकार की आधि-व्याधि से छुटकारा मिल सकता है।
धर्म के द्वारा ‘‘परलोक में सुख’’ मिलने की बात सच हो सकती है, पर इस मान्यता को नित्य-व्यवहार में अविवेकपूर्वक चलाये जाने के कारण ही उसमें इतनी अधिक बुराइयां आई हैं। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अनैतिकता आदि को प्रोत्साहन देने में यही मूल भावना कार्य कर रही हैं। उसमें उपरोक्त मान्यता का बहुत बड़ा हाथ है, पर अब यह निश्चित हो चुका है कि परलोक में यदि सुख मिल सकता है, तो उसका लाभ यहां क्यों नहीं मिल सकता? धर्म के द्वारा हमारा यह जीवन भी तो सुखमय होना चाहिए।
प्रश्न जितना गंभीर है, उतना ही उपयुक्त भी है; किंतु इसके लिए अपने व्यवहार, विचार और आचार की उत्कृष्टता को भी परखना पड़ेगा। धर्म का नित्य और अपरिवर्तनशील नीति-निर्देशक तत्त्व है—सद्गुण और सदाचार। इन्हीं पर धर्म का विशाल गढ़ निर्मित हुआ है। उपासना, सत्संग, स्वाध्याय, दान, तीर्थाटन आदि का आविर्भाव इन मूल प्रवृत्तियों को ही विकसित करने के लिए किया गया है; पर यह आवश्यकतायें ही इन दिनों नहीं हैं, इसलिए हमारे जातीय जीवन की इतनी अवनति हुई है। अपनी दुर्गति का मूल कारण यही है कि हम सद्विचार और सदाचरण के महत्त्व को भूलते जा रहे हैं। इस लोक का मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ भलाई का व्यवहार नहीं करेगा तो पारलौकिक जीवन में उसे सुख तथा शांति की उपलब्धि हो जायेगी, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। धर्म हमारे इस जीवन में ही शक्ति और सामर्थ्य पैदा कर देने की क्षमता रखता है, पर उसे हमारे व्यवहार में, विचार में और प्रत्येक गतिविधियों में सुंदर रूप में प्रतिष्ठित करना पढ़ेगा। जिस दिन से इस देश की सदाचरण वाली वृत्ति का जागरण होने लगेंगी, उस दिन से ही यहां अतीत की समृद्धियां पुनः लौटने लगेंगी और हम इसी धरती में ही सुख और संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इस महान् जागरण के लिए अब हमें उठना ही चाहिए। आत्म-हनन की परिपूर्ण प्रवंचना से हम बच सकें तो इसी धरती में स्वर्ग जैसा सुखोपभोग कर सकते हैं। आत्मा को दुर्गुणों द्वारा मार डालने से तो यह अवनति ही सुनिश्चित है, इसे आज इस देश में कष्टपूर्वक भोगा जा रहा है।
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- प्रजातंत्र की सफलता के लिए हम यह करें
- हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते?
- लोकमानस के प्रति शासनतंत्र का उत्तरदायित्व
- अनौचित्य के विरुद्ध समर्थ नैतिक क्रांति की आवश्यकता
- प्रगतिशीलता पर ही राष्ट्र का भविष्य निर्भर है
- आत्म-निरीक्षण की घड़ी आ पहुंची
- प्रगति के लिये नागरिक चेतना आवश्यक
- हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रहें
- राष्ट्रीय चरित्र को सुविकसित किया जाए
- हमारी आत्मा मर ही जायेगी क्या?
- प्रगति की दिशा में सही प्रयत्न
- राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में आपका योगदान
- जीवन का उजाला पक्षी भी प्रकाश में आए
- अंग्रेजी की अनिवार्यता हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध है
- छूत-अछूत का भेद क्यों
- अश्लीलता के अजगर से देश को बचाइए
- ग्रामोत्थान—राष्ट्र की आत्मा का उत्थान
- यह सर्वव्यापी भ्रष्टाचार रोका जाए
- खाद्यों में मिलावट की समस्या
- हम विदेशी सहायता के आश्रित
- हम शस्त्रों के लिए किसी के मोहताज न रहें
- बढ़ता मूल्य और गिरता स्तर कैसे रुके?
- व्यक्तिगत प्रगति और सामूहिक समृद्धि के लिए सामूहिकता अनिवार्य
- कृपया जनसंख्या और न बढ़ाइये
- मालिकों को जगाओ—प्रजातंत्र बचाओ
- प्रजा अपने कर्तव्यों से विमुख न हो
- चुनाव की पद्धति बदली जाए
- इतिहास की पुनरावृत्ति