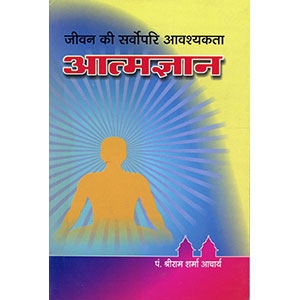जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान 
जीवनोद्देश्य से विमुख न हों
इस अनादि और अनंत काल के शाश्वत प्रवाह में न जाने वह कौन-सा अभागा क्षण था, जो मनुष्य को छूकर निकल गया, फलस्वरूप मनुष्य ने भोग-वासना की उपासना को अपना जीवन-लक्ष्य निर्धारित कर लिया।
क्या मनुष्य का जीवनलक्ष्य भोग-विथियों में भटकते रहना हो सकता है? किसी प्रकार भी तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा रहा होता, तो मनुष्य का निर्माण भी उसी प्रकार का हुआ होता जिस प्रकार अन्य पशुओं का। न उसमें बुद्धि होती, न विवेक और न ही आध्यात्मिक चेतना का विकास। संसार का यह सर्वगुणसंपन्न प्राणी मनुष्य भी यदि जीव-जंतुओं की भांति ही भोजन, आवास, निद्रा और मैथुन में रत रहकर ही सारा जीवन बिताता और मरकर चला जाता, तो फिर उसमें अंतर ही क्या रह जाता है?
प्राणियों के बीच एक-दूसरे से उनकी विशेषताओं की भिन्नताओं के पीछे निश्चित ही कुछ अर्थ और कुछ उद्देश्य निहित रहता है। परमात्मा की यह विशाल, व्यापक, नियमित तथा व्यवस्थित सृष्टि, किसी बाजीगर का निरुद्देश्य तमाशा भर नहीं है और न यह बालू से खेलते अबोध बच्चों की क्रीड़ा है कि वे मिट्टी से विविध प्रकार के आकार-प्रकार बनाते और यों ही कुतूहलवश बिगाड़ते रहते हैं। गाय-बैलों के सिर-सींग, शेर के पंजे, हाथी की सूंड़। वराह के वीर और पक्षियों के डैने होना, अपने पीछे एक सार्थक मंतव्य रखते हैं। यह यों ही निरर्थक की उपज एवं विभिन्नता नहीं है। यह बात दूसरी है कि हमारी मोटी बुद्धि इसके सूक्ष्म उद्देश्य को पूरी तरह समझ सकने में समर्थ न हो सके।
व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिष्कृत वाणी, बोलने और समझाने का गुण, सामाजिकता, पारस्परिकता, सहयोग, सौंदर्य, साहित्य, सहानुभूति, चिकित्सा, वाहन, मनोरंजन, न्याय, गृह, वस्त्र एवं आजीविका की सुविधा आदि की जो विशेषताएं मनुष्य को मिलीं और अन्य जीव-जंतुओं को नहीं मिली—परमात्मा के इस अनुग्रहाधिक्य का यह अर्थ तो कदापि नहीं हो सकता कि मनुष्य अपना जीवन इन विशेषताओं एवं सुविधाओं, इन पुरस्कारों एवं उपहारों को यों ही मिट्टी में मिलाकर अन्य पशुओं की तरह ही अपना जीवन बिताए और मर जाए। अवश्य ही मनुष्यों का जीवन उद्देश्य अन्य जीव-जंतुओं से भिन्न होना निर्धारित है।
मनुष्य जीवन-पद्धति की यह भिन्नता एक सोद्देश्य जिंदगी, एक ऊंची और परिष्कृत जिंदगी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। मानव जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वह शरीर की संकीर्ण परिधि से बाहर निकलकर व्यापक विभु की ओर बढ़े, नीचे स्तर से उठकर ऊपर अनंत की ओर अभियान करे। यदि वह सर्वगुणसंपन्न इस मनुष्य जीवन जैसे अलभ्य अवसर को पाकर भी अपनी आत्मा की संकीर्णता के कलुष से मुक्त करने का प्रयत्न न करे, तो यही मानना पड़ेगा कि हमने इस पावन प्रसाद का न तो समुचित मूल्यांकन ही किया और न परमात्मा की कृपा का समादर। इस मनुष्य शरीर को पशुओं जैसा यापन कर उसी श्रेणी का सिद्ध करने का अनुचित अपराध किया। आत्म-कल्याण, आत्म-मुक्ति एवं आत्म विस्तार की साधना में निरत रहकर न केवल यही एक अलभ्य अवसर खो दिया, वरन् आगे के लिए भी अपनी पात्रता असिद्ध कर दी और पुनः लाखों-करोड़ों वर्षों के लिए चौरासी लाख योनियों के कारावास की भूमिका तैयार कर ली।
शारीरिक वासनाओं की संकरी तथा असाध्य वीथियों से निकलकर यदि कुछ देर के लिए भी मन को मुक्त कर संसार के विस्तार तथा व्यापकता पर दृष्टिपात किया जाए, तो कोई कारण नहीं कि यह अनादि से लेकर अनंत तक फैला हुआ नीलाकश इसमें अवस्थित असंख्यों प्रकाशमान ग्रह, नक्षत्र, चांद एवं सूरज अपनी दिव्यता से हमारे उन्नत एवं व्यापक अभियान में सहायक न हों। कोई कारण नहीं कि इनका दर्शन, इनका विचार कुछ देर के लिए भी हमारे हृदय में व्यापकता की अनुभूति उद्बुद्ध न करे और हम इनके बीच अपने अंदर इन्हीं जैसी महानता तथा व्यापकता को अनुभव न करने लगें। किंतु कहां हम तो भोगों के रोगों से ग्रस्त अपने चारों ओर वासनाओं तथा एषणाओं की कारा निर्मित किए अपने को काल-कोठरी का बंदी बनाए पड़े हैं। हमें अवकाश ही कब मिलता है कि हम संकीर्णताओं से निकलकर इस अपार्थिव वैभव, इस व्यापक विभूति से तादात्म्य का प्रयास करें। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध और मोह आदि आत्म-विरोधियों का संग कर हम निविड़ अंधकार में भटककर अपने इस महान उद्देश्य की ओर से उदासीन होकर मनुष्य से पशु बने पड़े हैं और एक क्षण को भी यह सोचना नहीं चाहते कि अवसर निकला जा रहा है और हम अंत में पश्चात्ताप की अग्नि में जलने के लिए चूके जा रहे हैं।
नित्यप्रति सूर्योदय के समय से एक नया दिन आरंभ होता है और सूर्य अस्त होने तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नित्य ही आयु से एक मूल्यवान दिन कम हो जाता है। हम कभी नहीं सोचते कि हमने जिस दिन इन धरती पर जन्म लिया, उसी दिन से जीवन का ह्रास आरंभ हो गया है। बड़ी तेजी से क्षण-अनुक्षण, श्वास एवं प्रश्वास के साथ अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उस अंत की आर जिसकी स्थिति अथवा अवस्था का कोई आभास हमारे पास नहीं है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला हुआ यह छोटा सा अवसर, यह गिना-चुना समय यों ही व्यर्थ में नष्ट हुआ जा रहा है और हम उसके लिए कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं।
हम नित्य ही जन्म-मृत्यु, जरता-क्षरता, रोग-शोक, आपत्ति, विनाश, काल एवं अकाल मृत्यु के विचार प्रेरक तथा जगा देने वाले दृश्य देखते-सुनते ही रहते हैं, किंतु हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। विषय-वासनाओं, कामनाओं, एषणाओं, भोग तथा लोलुपता ने हमें इस सीमा तक मोहग्रस्त बना दिया है कि हम विचार, विवेक और बुद्धि के रूप में अंधे ही हो गए हैं। सांसारिकता के प्रमाद में इस सीमा तक विस्मृत हो गए हैं, डूब गए हैं कि एकआध घड़ी एकांत में बैठकर विचार कर सकें कि हमको यह विचित्रतापूर्ण मानव शरीर क्यों मिला? इसका उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं? कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? इस प्रकार की कल्याणकारी भावना, जिज्ञासा अथवा उत्सुकता की चेतना से हम सर्वथा अपरिचित ही हो गए हैं।
एक तिनके की तरह हम चेतनाहीन होकर समय के प्रवाह, विकृतियों के वेग में, संसार की अबूझ परंपरा—जन्म लेना, जीना और मर जाना, के साथ बहे चले जा रहे हैं। इंद्रिय भोग, पदार्थ पूजा, अधिकार, पुत्र-कलत्र, धन-धान्य आदि दायित्व एवं परतंत्रताजन्य वस्तुओं को लक्ष्य बनाकर दिन-रात इन्हीं में मरते-खपते चले जा रहे हैं। जब अंतकाल आता, चेतना जागती और बुद्धि प्रश्न करती है, तब हम अपनी भूल समझते और छटपटा उठते हैं, किंतु तब तक जीवन की हाट उठने लगती है और हम उस सबको ज्यों-का-त्यों यथास्थान छोड़कर खाली हाथ मलते हुए किसी अनजान दिशा की ओर चल देते हैं। वह कुछ भी न तो हमारे साथ जाता है और न काम ही आता है, जिसका हमने सुर-दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करके बड़े उत्साह से संचय किया था। विशाल वैभव, अपार धन-धान्य, पुत्र-कलत्रादिक संचय तथा संसार की सारी परिस्थितियां हमारे सामने बनी रहती हैं। जिनको हम अपना कहते और जिनके लिए प्राण देते रहते हैं, कोई भी काम नहीं आते, हम अपनी मोहमयी भूल के पश्चात्ताप में जलते हुए परवशता के परों से बंधे उड़ ही जाते हैं। उस समय की वह व्याकुलता, वह व्यग्रता और शोक-संताप या तो वह ही समझ सकता है, जो भुक्तभोगी रहा है अथवा वह समझेगा जो आज उसी भूल का प्रतिपादन करता हुआ सोचने-समझने की आवश्यकता नहीं समझता।
जीवन के प्रति विश्वास एवं आस्था रखना अच्छी बात है। तथापि जिंदगी कितनी ही लंबी और विश्वासपूर्ण क्यों न हो, जीवनलक्ष्य की महानता को देखते और संसार की नश्वरता को समझते वह सदैव छोटी तथा अविश्वस्त ही है। इसका एक-एक क्षण मूल्यवान है। हर बीते हुए क्षण की क्षति पूरी नहीं की जा सकती, किसी आए हुए क्षण को व्यर्थ नहीं किया जा सकता। लक्ष्य की दिशा में ही उपयुक्त किया हुआ क्षण हमारा सार्थक तथा सहयोगी हो सकता है, अन्यथा जीवन के पचास-सौ साल क्या हजार और लाख-लाख वर्ष भी निरर्थक एवं निरुपयोगी ही सिद्ध होते हैं।
अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को ही उन्नति और सफलता का प्रतीक मान लेता है, किंतु मनुष्य शरीर, बल, बुद्धि, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य अथवा पद-प्रतिष्ठा के क्षेत्र में क्या न हिमालय की तरह ऊंचा और सागर की तरह गहरा हो जाए, किंतु जब तक उसमें आत्म–संपदा का अभाव है, आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है, तब तक वह निर्धन तथा निम्नकोटि का ही माना जाएगा। आत्मोन्नति एवं आध्यात्मिक उपलब्धि ही वह वास्तविक उन्नति एवं विकास है, जिसे प्राप्त कर यह मानव जीवन धन्य तथा सार्थक होता है। भौतिक विभूतियों की चमक मरुस्थल की उस मरीचिका से अधिक कुछ भी तो नहीं है, जो कि आकर्षक तो बहुत होती है किंतु न तो आत्मा की प्यास बुझा सकती है और न हृदय को संतोष दे सकती है।
यह बात सोचना-समझना भूल होगी कि मानव जीवन में भौतिक पदार्थों का कोई मूल्य या महत्त्व नहीं है। मनुष्य का शरीर पार्थिव है, उसे चलाने तथा बनाए रखने के लिए भौतिक पदार्थ की नितांत आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र तथा निवासादिक आवश्यकताओं की आपूर्ति में जीवन चलना ही कठिन हो जाएगा। किंतु इनका महत्त्व केवल उस सीमा तक ही है कि ये मानव जीवन के उद्देश्य की पूरक मात्र ही बने रहें, स्वतः लक्ष्य न बन जाएं। शरीर-रक्षा और अपने जीवन की असुविधा दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपार्जन एवं इनकी प्राप्ति में आवश्यक समय तथा श्रम देने के उपरांत जो शक्तियां और जो अवसर शेष बचे, उन्हें परम लक्ष्य की ओर जाने में ही लगाना बुद्धिमानी है। भौतिकता के साथ अपना समग्र जीवन बेच देने का अर्थ यही होगा कि हम अपने उद्देश्य की दिशा में भटककर गलत रास्ते पर चल निकले हैं। जो साधन था, वह हमारा साध्य बन गया है। ऐसी दशा में यथाशीघ्र अपना सुधार कर लेना ही कल्याणकारी माना जाएगा।
जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी रचना के चरमोत्कर्ष लक्ष्य तक तब ही पहुंच पाता है, जब वह अपने अभिलेखन में कला एवं सौंदर्य का समुचित समन्वय कर लेता है। कला-विहीन सुंदर रचना अथवा कलापूर्ण असुंदर रचना दोनों ही अपने में अपूर्ण एवं अवांछनीय होने से कलाकार को अपने चरमोत्कर्ष के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाती। उसी प्रकार भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समुचित समन्वय ही मनुष्य को उसके आत्मोत्कर्ष के लक्ष्य तक ले जा सकता है। यदि कोई भौतिक आवश्यकताओं की सर्वथा उपेक्षा कर आध्यात्मिक चिंतन अथवा साधना में लगा रहे, तो आवश्यकताओं की पीड़ा से उसका चित्त अस्थिर रहेगा और शरीर जवाब दे देगा, जिसका फल अनानुभूति के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की आध्यात्मिक साधना उसके लिए मृत्यु की तरह कष्टदायक बन जाएगी। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक साधना से विरत होकर केवल भौतिक भोगों की ही उपासना की जाती रहे, तो भी मानवीय लक्ष्य दूर से दूरतर होता चला जाएगा। दोनों का समुचित समन्वय ही उद्देश्य-पूर्ति का कारण बन सकता है, जिसका अनुपात कम-से-कम पच्चीस और पचहत्तर का ही होना चाहिए। उससे कम अनुपात में लक्ष्यप्राप्ति के लिए अनेक जन्म-जन्मांतरों तक प्रयत्न एवं प्रतीक्षा करनी होगी।
येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम्
महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी समस्त संपत्ति को दोनों पत्नियों में बराबर बांटकर गृह त्याग के लिए उद्यत हुए। मैत्रेयी को संतोष नहीं हुआ और आखिर वह पूछ ही बैठी—‘‘भगवन! क्या मैं इस सबको लेकर जीवन-मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकूंगी?’’ ‘‘क्या मैं मर जाऊंगी या आत्मतोष प्राप्त कर सकूंगी?’’ महर्षि ने अपने चिंतन का क्रम तोड़ते हुए कहा—‘‘नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। साधन-सुविधा संपन्न सुखी जीवन जैसा अब तक तुम्हारा रहा, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा, अन्य सांसारिक लोगों की तरह ही तुम भी अपना जीवन सुख-सुविधा के साथ बिता सकोगी।’’
मैत्रेयी का असंतोष दूर नहीं हुआ और वे बोलीं—‘‘येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम् ।’’ (बृहदारण्यकोपनिषद् 4,5,6) ‘‘जिससे मुझे अमृतत्व प्राप्त न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? देव! मुझे यह सुख-सुविधा संपन्न सांसारिक जीवन नहीं चाहिए।’’
‘‘तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, मैत्रेयी?’’ महर्षि ने पूछा। मैत्रेयी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका हृदय संपूर्ण भाव से उमड़ पड़ा उस दिन। मैत्रेयी ने महर्षि के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा—
‘‘असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतंगमय। आविरावीर्मा एधि रुद्र यत्ते दक्षिण मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ।’’
‘‘हे प्रभो! मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत्यु की ओर गति प्रदान करो। देव! हे प्रकाश! आप चिर प्रकाश बनकर मेरे जीवन में प्रकाशित हो उठें। रुद्र बनकर मेरे समस्त पापरूपी अंधकार का नाश कर दें। अपने प्रेम स्वरूप आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें, जिसकी छाया में, मैं चिरकाल तक परित्राण प्राप्त कर सकूं।’’
मैत्रेयी ने महर्षि के सान्निध्य में सुख-समृद्धि और संपन्नता का जीवन बिताया था, किंतु उसके अंतर का यह प्रश्न अभी तक अधूरा था। उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया था।
हम जीवन भर नाना संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव एकत्र करते हैं। आश्रम, धन, नाना पदार्थ, बहुमूल्य सामग्री जुटाते हैं और अंतर में स्थित मैत्रेयी को सौंपते हुए कहते हैं—‘‘लो! इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा।’’ अनेकानेक सामग्री हम जुटाते हैं, किंतु अंतर में बैठी हुई मैत्रीय कहती ही रहती है—‘‘येनाहं नामृतस्यां किमहं तेन कुर्याम् ।’’ इन सब सामग्रियों में जीवन के शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं मिलता और आत्म–चेतना निरंतर छटपटाती रहती है। उस महत्त्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति के लिए जो उसे सत्य, ज्योतिर्मय अमृतत्व की प्राप्ति करा सके, सब ओर से उसे परित्राण देकर आनंदमय बना सके।
मैत्रेयी चाहती थी कि उस परमतत्त्व का साक्षात्कार, एकानुभूति, नित्य दर्शन, जो सत्य, ज्योतिर्मय स्वरूप है, जो उसके जीवन का चिर प्रकाश बने। रुद्र बनकर उसके समस्त पाप-तापों को नष्ट कर दे और उसे परित्राण देकर निर्भय बना दे।
मैत्रेयी ने अपने अनुभव की कसौटी पर जान लिया था, संसार और इसके सकल पदार्थ, संबंध, नाते, रिश्ते मरणशील हैं, इनका पर्यवसान अंधकार और असत्य में ही होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक पाप-तापों की पीड़ा जीव को सदा ही अशांत-भयभीत बनाए रखती है।
मनुष्य नाना पदार्थ, उपकरणादि संग्रह करता है। धन-संपत्ति जुटाता है। बड़े-बड़े महल बनाता, देह को नाना भांति सजाता-संवारता है। रात-दिन इन्हीं को आधार बनाकर जुटे रहने से इनके प्रति मनुश्य में एक तह की आसक्ति एवं ममता उत्पन्न हो जाती है। धीरे-धीरे यह अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मनुष्य इन्हीं उपकरणों, सामग्री, संबंधों को सब कुछ मान इन्हीं का अवलंबन लेकर चलने लगता है। किंतु संसार के नियम के अनुसार ये मिट्टी के घरोंदे क्षण-क्षण में गिरते-पड़ते रहते हैं। परिवर्तित होते रहते हैं। संसार और इसके पदार्थ बनते-बिगड़ते रहते हैं। कोई भी तो स्थिर नहीं रहता। मनुष्य का शरीर ही वृक्ष के पत्ते की तरह एक दिन झड़ जाता है। वह भी स्थिर नहीं रहता। जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब ही तो असत्य है, मरण-धर्मा है, अंधकारमय है।
मनुष्य इनका अवलंबन लेकर क्षण-क्षण इनके वियोग, रूपांतरण-परिवर्तन के साथ-साथ ही मृत्यु का अनुभव करता है। जिसे सत्य मान लिया गया था, वे तो स्वप्न की तरह असत्य सिद्ध होते हैं। कृत्रिम प्रकाश के बुझ जाने पर अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। इससे क्षण-क्षण मृत्यु के असत्य और अंधकार में ही भटकता रहता है। भय, आशंका, क्लेश, पाप, ताप उसे क्षण भर भी तो स्थिर नहीं रहने देते। आवर्तनशील श्रम चलता ही रहता है और इसका कोई अंत ही नहीं होता।
इसीलिये मैत्रेयी को इन सब वस्तु, पदार्थ, संपत्ति, समृद्धि से परे किसी ऐसी वस्तु की अभिलाषा थी, जो इस तरह के मरणधर्म, प्रत्यावर्तन, स्वप्नवत असत्यता, परिणाम में अंधकार से सर्वथा मुक्त हो। जिसे प्राप्त करने के बाद फिर छोड़ने या बदलने का कोई प्रश्न ही उपस्थित न हो। जो मृत्यु से अतीत, सत्य, ज्योतिर्मय, दिव्यरूप हो। ऐसा अमृतत्व चाहती थी मैत्रेयी।
लेकिन हम शक्ति और युक्ति संसार के पदार्थों में सत्य ढूंढ़ते हैं, नाप-जोख करते हैं। नाना साज-सामान एकत्र करते हैं और अंतर में विराजमान मैत्रेयी से कहते हैं—‘‘लो देवि! इन्हें ग्रहण करो और सुखपूर्ण जीवन बिताओ।’’ किंतु वह हर बार अपना असंतोष प्रकट करते हुए पूछती है, क्या इससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो सकेगी?
‘‘नहीं?’’ तो फिर जो मैं चाहती हूं, (बृह0 4.5.4) जिससे मुझे अमृतस्वरूप की उपलब्धि न हो, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? और यह नित्य-निरंतर ही अश्रुपूरित नेत्रों और व्याकुल हृदय से प्रार्थना करती है—
‘‘असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योर्गिमय, मृत्योर्माऽमृतंगमय (बृह0 1.3.28)। आविरावीर्मा एधि (ऐतरेयोपनिषद् शांतिपाठ) रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ।’’ (श्वेताश्वतर0 4.21)
‘‘हे चिरंतन सत्य! मेरे अंतर और बाह्य सर्वत्र ही विराजमान सत्य! मुझे असत्य की सीमा से निकालकर अपने में मिला लो। जब के असत्य परदों को हटाकर अपने सत्य स्वरूप भवन में ले चलो, जहां ‘‘आप हैं।’’ आपके सिवाय कुछ भी न हो।’’
‘‘ज्योतिषां यद् ज्योतिः’’ सर्व लोकों में ज्योतियों की भी पर ज्योति। कोटि-कोटि सूर्य सम आप की परम ज्योति व्याप्त है। हे ज्योतिर्मय! अपने पावन स्पर्श से मुझे भी ज्योतिर्मय बना दें, जिससे अंधकार के समस्त परिवेष्टनों से मुक्त होकर मैं भी ज्योतिर्मय बनूं।’’
‘‘हे अमृत रस! परमानंद के धाम! सर्वत्र आप ही अजर-अमर-अविनाशी बनकर व्याप्त हैं। यह जगत् आप में ही धारण, पोषण, विनाश प्राप्त करता है, किंतु आप सदा-सदा गंभीर, स्तब्ध, एकरस बने रहते हैं। आपका कोई रूप, सीमा, आयु नहीं। अपने इस अमृत स्वरूप में मिलाकर मुझे भी अमर्त्य बनाएं।’’
‘‘हे प्रकाश! मुझे अपने प्रकाश से जगमग-जगमग कर दो। अपनेपन, अहंकार, राग, आसक्ति के समस्त अंधकार का उच्छेद करके पूर्णरूपेण प्रकाशमय कर दो।’’
‘‘हे रुद्र! अपने प्रचंड ताप से मेरे समस्त पापों को भस्मीभूत कर आदिपाप हों उन्हें अपने रुद्र ताप से नष्ट कर दो, तब आपके आलोक प्रकाश की निर्विकारी सत्ता ही मुझमें शेष रहेगी। हे प्रभो! आप अपने प्रसन्न, मधुर, आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करो। हे देव! तब मैं आपका ही निवास बनकर सर्व ओर से परित्राण पा सकूंगी।’’
अंतर में विराजमान मैत्रेयी रूपी अंतरात्मा की इस प्रार्थना को हम एकाग्रता के साथ सुनें। उसके स्वरों में स्वर मिलाकर गाएं। प्रबल जिज्ञासा, उत्कृष्ट इच्छा, अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ ही हमारी यह प्रार्थना किसी तरह की सौदेबाजी, लेन-देन या संजोकर रखने की बात न हो। संसार के बीच में विचरण करते हुए हम उसी को ग्रहण करें, जो हमारी आत्मा की चिर इच्छा को पूर्ण करे। उस सत्य अमृत-ज्योति की प्राप्ति कराए। जो हमें अमर्त्य प्रदान न करे उसे छोड़ते जाएं।
‘‘येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम् ।’’ (बृह0 4.5.4) यह हमारा जीवन मंत्र बन जाए।
***
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- आत्म्-सत्ता और उसकी महान महत्ता
- हमारा जीवन लक्ष्य, आत्म-दर्शन
- जीवनोद्देश्य से विमुख न हों
- शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें
- अमर हो तुम, अमरत्व को पहचानो
- मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए
- मनुष्य और उसकी महान शक्ति
- जीवन का दूसरा पहलू भी भूलें नहीं
- आत्मा की पुकार अनसुनी न करें
- आत्मा की पुकार सुनें और उसे सार्थक करें
- आत्म-ज्ञान की आवश्यकता क्यों?
- आत्म-ज्ञान से ही दुःखों की निवृत्ति संभव है
- सत्यं, शिवं सुंदरम्—हमारा परम लक्ष्य
- शक्ति के स्रोत—आत्मा को मानिए
- आत्मा को जानिए
- आत्म-शक्ति का अकूत भंडार
- शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है
- सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे
- चेतन, चित्त—न, चिंतन
- आत्मा और परमात्मा का संबंध
- ईश्वर अंश जीव अविनाशी
- परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो
- अहं और उसकी वास्तविक सत्ता
- बिंदु में सिंधु समाया
- अपूर्णता से पूर्णता की ओर
- क्या आत्—कल्याण के लिए गृहत्याग आवश्यक है?
- आत्म-बल हमारी सबसे बड़ी वैभव-विभूति
- जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ
- आत्म-विकास के लिए व्रत पालन की आवश्यकता