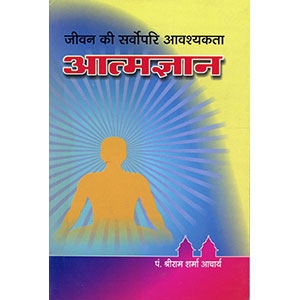जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान 
अपूर्णता से पूर्णता की ओर
यह सब कुछ अपूर्ण है। विश्व की कण-कण अपूर्णता से पूर्णता की ओर चल रहा है। प्रकृति अपूर्ण है, इसलिए उसके परमाणु गतिशील चंचल होकर पूर्णता की खोज में दौड़ रहे हैं। मानव समाज अपूर्ण है, उसे जो कुछ मिला है, उससे उसे अपना काम चलता नहीं दीखता, उसमें उसे संतोष नहीं। अपूर्णता में संतोष हो भी कैसे सकता है? इसलिए वह अधिक मात्रा में, अधिक उत्कृष्ट वस्तुएं एवं परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हैं। आत्मा अपूर्ण है। वह परमात्मा का एक अणु मात्र ही तो है। इतने भर से उसे संतोष कैसे हो? वह अन्य सजातीयों के साथ मिलकर एक बड़ी सत्ता बनना चाहता है, इसलिए दूसरों को प्रेम करता है। प्रेम के, आत्मीयता के आधार पर ही दूसरों को अपने में मिलाकर अधिक विस्तार की अनुभूति हो सकती है। आत्मा की भूख निरंतर प्रेम की है। वह प्रेम चाहता है, अधिक विस्तार में, अधिक उच्चकोटि का प्रेम उपलब्ध किस प्रकार हो, यह प्यास उसे निरंतर लगी रहती है और इस तृष्णा को बुझाने के लिए उससे जो कुछ बन पड़ता है, वह निरंतर करता रहता है।
उपनिषदों में परमात्मा को तीन भागों में विभक्त बताया है। एक जगत में, एक मानव समाज में, एक आत्मा में। उसे शान्तम्, शिवम्, अद्वैतम् कहा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए ही विश्वव्यापी प्रक्रिया चल रही है। जगत में जो अशांति है, चंचलता है, गतिशीलता है, वह इसलिए है कि इस मंजिल को पार करके शांति रूपी प्रकाश उपलब्ध हो। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, अणु, परमाणु सभी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। यह कहां जाना चाहते हैं? इनकी यात्रा का लक्ष्य क्या है? निश्चय ही यह अशांति-शांति की तलाश में चल रही है, जब सृष्टि का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, तो प्रत्येक अणु पिंड शांत होकर परब्रह्म में लीन होकर अनंत शांति का अनुभव करने लगता है। प्रलय काल में यह जगत ऐसी ही शांति का अनुभव करता है।
मानव समाज का लक्ष्य शिवम् है। शिव अर्थात् कल्याण। मानव समाज का, मानव मनोभूमि का गठन इस प्रकार का है कि इसमें अनेक अभाव, दोष, अमंगल, कष्ट एवं दुःख भरे दीखते हैं। हर मनुष्य अपनी किसी-न-किसी समस्या को लेकर दुःखी और असंतुष्ट है। इन अभावों और असंतोषों की निवृत्ति के लिए ही वह अपनी मति के अनुसार नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। उसे सुख चाहिए। अधिक मात्रा में अधिक अच्छा, अधिक टिकाऊ सुख की उपलब्धि के लिए समाज में असाधारण हलचल होती रहती है। उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनाश की समस्याएं उलझी रहती हैं, उन्हें सुलझाने के लिए प्रिय और अप्रिय कर्म एवं अकर्म होते रहते हैं। शिव के रूप में, कल्याण के रूप में, ईश्वरीय प्रकाश समाज में मौजूद है। उसे जब उपलब्ध कर लिया जाता है, तब स्वर्गीय परिस्थितियों का भान होता है, उन्हें पाकर मनुष्य अपने आप को देवता के रूप में अनुभव करता है।
आत्मा के लिए जो प्रकाश प्राप्त करने योग्य है, वह है एकता का अद्वैत। जो आत्मा जितना ही अपने-पराये, मेरे-तेरे के फेर में है, दूसरों को अपने से जितना ही भिन्न मानता है, वह उतना ही दुखी है। उसे उतना ही दूसरों के प्रति भय और संदेह बना रहता है। प्रेम का मिलन जितना-जितना बढ़ता जाता है, उतना ही वह द्वैत समाप्त होने लगता है, जो अनेक प्रकार की आशंकाओं और उद्वेगों का मूल है, मां और बेटे में जब आत्मीयता पैदा हो जाती है, तो दोनों में से किसी को भय नहीं रहता कि दूसरा मेरा कोई अनिष्ट करेगा, वरन् एक को देखकर दूसरे को प्रसन्नता होती है, हिम्मत बंधती है, संतोष और सुख प्राप्त होता है। पति यदि अपनी जेब में छुरी या पिस्तौल रखे हुए हो, तो उसकी पत्नी का उससे जरा भी भय नहीं लगता। कसाई दिनभर जीवों की हत्या करते हैं, पर उनके बच्चे उनके हाथ में छुरा लिए रहने पर भी नहीं डरते। क्योंकि प्रेम का प्रकाश जहां फैलता है, वहां अविश्वास और भय का अंधकार ठहर ही कहा सकता है?
प्रेम का नाम अद्वैत है। इसे ही भक्ति कहते हैं। ईश्वर को अवलंब बनाकर जो भक्ति की जाती है, वह उस ईश्वर तक सीमित नहीं रह सकती, जो उपासना की सुविधा के लिए एक प्रतिमा या प्रतीक के रूप में कल्पित की गई थी। पहलवान मुगदर की सहायता से अपनी भुजाओं का बल बढ़ाता है। वह भुजबल जीवन के विस्तृत क्षेत्र में अनेक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा नहीं है कि वह भुजबल केवल मुगदर उठाने तक ही सीमित रहे। यदि कोई पहलवान भारी मुगदर तो उठा लेता हो, पर उसकी भुजाएं और कुछ पराक्रम करने में असमर्थ हों, तो लोग उसे पहलवान नहीं कहेंगे, वरन् कोई जादूगर समझकर उस मुगदर उठाने वाले की क्रिया में कोई चालाकी होने का संदेह करने लगेंगे। यही बात प्रेम के संबंध में भी है। ईश्वर भक्त अपने प्रेमभाव को बढ़ाने के अभ्यास के रूप में भक्ति की साधना करता है। इसमें जितनी ही सफलता मिलती जाती है, उसी अनुपात में आत्मा का प्रेम प्रकाश प्राणिमात्र के ऊपर फैलना आरंभ हो जाता है। उसे सब कोई अपनी प्रेमी ही दीखते हैं। प्रेमी भी नहीं, आत्मीय ही लगते हैं। फिर उसे सब कुछ अपना ही, अपने में ओत-प्रोत ही दीखने लगता है। यही अद्वैतभाव है। वेदांत सिद्धांत में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर इसी आत्मीयता और एकता का शिक्षण किया गया है, मुक्ति का यही उपाय है। तुच्छता के, संकीर्णता के, अनुदारता के, वासना ओर तृष्णा के, लोभ और मोह के बंधन जितने ही शिथिल होते जाएंगे, उतनी ही मुक्ति समीप आती जाएगी। द्वैत में ही बंधन और अद्वैत में ही मुक्ति है। प्रेम को परमात्मा कहा गया है—रसौ वै सः—वह परमात्मा प्रेम स्वरूप है, अपनी अंतरात्मा यदि स्वार्थ ओर मोह से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम को अपना ले, तो उसके लिए परमात्मा प्रत्यक्ष ही है। उसकी मुक्ति उसके साथ ही है।
जिस प्रकार द्वैत को घटा या मिटाकर आत्मा अद्वैत तत्त्व की, प्रेमास्पद परमात्मा की, समीपता का असीम आनंद इसी जीवन में अनुभव कर सकता है और जीवन मुक्ति के सुख को प्रत्यक्ष कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए यह भी सरल है कि वह स्वर्गीय भूमिका में विचरण करने वाले देवत्व से अपने आप को ओत-प्रोत अनुभव करे। दुःखों और अभावों से उत्पन्न होने वाली खिन्नता पर विजय प्राप्त करके ही जीवनयापन क्रम की परेशानी एवं नीरसता को हटाया जा सकता है।
हमें यह मानकर चलना होगा कि दुःख भी मानव जीवन का एक तथ्य है, उससे रहित होकर जी सकना किसी के लिए संभव नहीं। वह अनिवार्य ही नहीं, उपयोगी एवं आवश्यक भी है। सुख की ही तरह वह भी जीवन के विकासक्रम में सहायक होता है। केवल सुख-ही-सुख प्राप्त हो, तो वह उसकी उपयोगिता भी न समझ सकेगा और वह एक भार मात्र बनकर रह जाएगा। पकवान एवं मिष्ठान्न का आनंद उसे आता है, जिसे रूखी-सूखी रोटियों से भी पाला पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सदा मिठाई और पकवान ही खाता रहे, तो उसके लिए उनमें क्या रस हो सकता है? गरीबी की अनुभूति के साथ धन-लाभ का सुख संबंधित है। यदि कोई बालक ऐसे घर में जन्मे जहां सोना-चांदी के ढेर जमा रहते हों, तो उसे थोड़ा और धन-लाभ होने पर क्या प्रसन्नता होगी? यदि धनप्राप्ति के सुख का आस्वादन करना हो, तो गरीब की परिस्थितियों में से गुजरना आवश्यक है।
सफलता में, विजय में और उन्नति में आनंद उपलब्ध हो सके, इसके लिए असफलता, पराजय, अवनति के झकझोरे आवश्यक हैं। स्वास्थ्य भी परमात्मा की कोई देन है, इसे रोगी होने पर ही कोई व्यक्ति भली प्रकार समझ सकता है, अन्यथा एक बलवान आदमी तो अपने नीरोग शरीर का कोई मूल्य क्या समझेगा? उसके लिए तो वह एक साधारण-सी अनायास प्राप्त हुई तुच्छ-सी चीज है। दुःख एक कसौटी है जिस पर कसकर सुखों के मूल्य को समझ सकना संभव होता है।
यदि हमारे हाथ में दुःख का पात्र न होता, तो परमात्मा की दया-भिक्षा हम किसमें प्राप्त करते? अपूर्णता यदि न होती, अभाव यदि न रहते, तो पराक्रम और पुरुषार्थ के जाग्रत होने का अवसर ही न आता और उसके बिना जीव की उन्नति का क्रम ही रुक जाता। इस विश्व में स्वर्गीय पदार्थों एवं परिस्थितियों की कमी नहीं, पर वे प्राप्त उन्हीं को होती हैं, जो उनका मूल्य कष्ट सहन करके चुकाने को तैयार होते हैं। साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। विद्या पढ़ने, धन कमाने, बलवान बनने, सुसंस्कृत होने के लिए हर किसी को कष्टसाध्य उपायों का अवलंबन करना होता है, जो इससे बचना चाहते हैं, वे अपनी पात्रता को सिद्ध नहीं कर पाते और उन दिव्य उपहारों से वंचित रह जाते हैं, जो केवल पराक्रमी विजेताओं के लिए ही सुरक्षित रखे रहते हैं।
अभावों और कष्टों को एक प्रेरक शक्ति एवं उद्दीपक अग्नि के रूप में, अपने पुरुषार्थ के लिए उपस्थित हुई चुनौती के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा जो लोग निराश, खिन्न एवं व्यग्र हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अपने आप को अभागा मानने लगते हैं, वे दुःख के देवता का अपमान करते हैं। सुख, बुखार के दैत्य की तरह है, जो जब उतरता है, तो देह थकी-मांदी-सी लगती है, पर दुःख उस राजा की तरह है, जो जहां ठहरता है, वहीं कुछ-न-कुछ उपहार देकर जाता है। संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम छोड़ा है, उनमें से हर एक को दुःखों की अग्नि में तपना पड़ा है। योगीजन इसे स्वेच्छापूर्वक अंगीकार करते हैं। अपरिग्रह, तितिक्षा और तपस्या की अग्नि में अपने को तपा-तपाकर अधिक उज्ज्वल और प्रकाशवान बनाते चलते हैं। यदि वे इस मार्ग पर न चलें, विलासी और ऐश-आराम का जीवन व्यतीत करें, तो निश्चय ही उन्हें उन आध्यात्मिक लाभों से वंचित रहना पड़ेगा, जो तपस्वी और योगियों को प्राप्त होते हैं।
ईश्वरीय प्रकाश को तीनों दिशाओं से हमें ग्रहण करना होगा। अद्वैत भावना का, प्रेमतत्त्व का विस्तार करके आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी। समाजव्यापी अभावों और दुःखों को, पराजयों एवं असफलताओं को, हानि-लाभ, मान-अपमान, राग-द्वेष आदि द्वंद्वों को एक कटु आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उनसे खिन्न होने की अपेक्षा अपने मानसिक एवं बाह्य क्षेत्र में अधिक सावधान होने की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम दुःखों को भी सुख के समान ही जीवन का एक आवश्यक एवं उपयोगी तत्त्व मान लें और उससे मन को गिरने देने की भूल न करें, तो हमारा सामाजिक जीवन स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण हो सकता है।
प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ अपनी अपूर्णता दूर करके पूर्णता प्राप्त करने के लिए तीर की तरह दौड़ा जाता है। ऐसी दशा में किसी पदार्थ की यहां तक कि शरीर की भी एक स्थिति में, एक आधिपत्य में रहने की आशा कैसे की जा सकती है? यह सभी कुछ दौड़ रहा है, यह सभी कुछ चंचल है। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। रूप, विवेक, धन, यश, ऐश्वर्य, सत्ता, बुद्धि, चातुर्य यह सभी चंचला लक्ष्मी के अंग हैं। परिवार के परिजन, मित्र और कुटुंबी, स्त्री और पुत्र, स्वजन और संबंधी इसमें से किसका शरीर, किसका मन कब तक अपने को प्रिय लगने की, स्थिर रहने की स्थिति में रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। फिर इस दौड़ती हुई रेल के पीछे गले में रस्सी बांधकर घिसटते चलने से क्या लाभ?
इन तीनों तथ्यों को यदि समझ लिया जाए, तो जगत में अशांत, चंचल स्वभाव से परिचित होकर मोह-बंधनों से छूट सकना, हमारे लिए संभव हो सकता है। दुःखों के डर से जो नारकीय यातनाएं उठानी पड़ती हैं, उन्हें स्वर्गीय परिस्थिति में बदला जा सकता है, द्वैत भावना से उत्पन्न परायेपन का अज्ञान जो जीव को ईर्ष्या, द्वेष एवं पाप, ताप से जलाता रहता है, उससे भी निवृत्ति हो सकती है।
ईश्वरीय प्रकाश शांत, शिवम् और अद्वैत है। यदि हम चाहें, तो उसे प्राप्त कर सकते हैं और मानव जीवन को धन्य बन सकते हैं।
***
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- आत्म्-सत्ता और उसकी महान महत्ता
- हमारा जीवन लक्ष्य, आत्म-दर्शन
- जीवनोद्देश्य से विमुख न हों
- शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें
- अमर हो तुम, अमरत्व को पहचानो
- मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए
- मनुष्य और उसकी महान शक्ति
- जीवन का दूसरा पहलू भी भूलें नहीं
- आत्मा की पुकार अनसुनी न करें
- आत्मा की पुकार सुनें और उसे सार्थक करें
- आत्म-ज्ञान की आवश्यकता क्यों?
- आत्म-ज्ञान से ही दुःखों की निवृत्ति संभव है
- सत्यं, शिवं सुंदरम्—हमारा परम लक्ष्य
- शक्ति के स्रोत—आत्मा को मानिए
- आत्मा को जानिए
- आत्म-शक्ति का अकूत भंडार
- शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है
- सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे
- चेतन, चित्त—न, चिंतन
- आत्मा और परमात्मा का संबंध
- ईश्वर अंश जीव अविनाशी
- परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो
- अहं और उसकी वास्तविक सत्ता
- बिंदु में सिंधु समाया
- अपूर्णता से पूर्णता की ओर
- क्या आत्—कल्याण के लिए गृहत्याग आवश्यक है?
- आत्म-बल हमारी सबसे बड़ी वैभव-विभूति
- जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ
- आत्म-विकास के लिए व्रत पालन की आवश्यकता