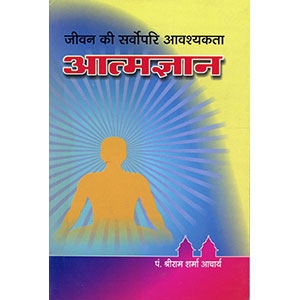जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान 
सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे
आत्मा के उद्धार के लिए शास्त्रों और उपनिषदों में काफी साधन और ज्ञान पड़ा हुआ है, किंतु साहित्य का स्वाध्याय कर लेने, उसका ज्ञान बढ़ाकर उपदेश कर लेने से किसी को आत्म-साक्षात्कार नहीं हो जाता। गीताकार का स्पष्ट निर्देश है—
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य—
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ।। —मुण्डको0 3.2.3
‘‘यह आत्मा बहुत उपदेश कर लेने से नहीं मिला जाता। बहुत ज्ञान और शास्त्रों के सुन लेने से भी वह प्राप्त नहीं होता। वह आत्मा को वरण करने से ही जाना जा सकता है।’’
आत्मा सत्य है, शाश्वत और नित्य है, शक्ति का स्वरूप है। पर जब तक वह सांसारिक आत्म-कल्पनाओं से विमुक्त नहीं हो जाती, वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हो सकती। शास्त्रों का, सत्साहित्य का स्वाध्याय और ज्ञान-संवर्द्धन भी इस कार्य में सहायक है, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमान लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए भी देखे जाते हैं। ज्ञान के द्वारा यदि आत्म-लाभ संभव रहा होता, तो अनेक पाश्चात्य दार्शनिक बहुत ज्ञानवान हुए हैं। वे सब आत्मज्ञानी रहे होते और यदि इन देशों में थोड़े भी आत्मज्ञानी रहे होते, तो आज उनकी दशा ही भिन्न होती। भौतिक दृष्टि से समृद्ध बनकर भी बुराइयों का जाल फैलाकर और उपदेश देकर तब न दूसरों के लिए अभिशाप बनते, वरन् स्वयं भी आध्यात्मिक सुखों का रसास्वादन कर रहे होते।
औरों को उपदेश करने की अपेक्षा अपना उपदेश आप कर लिया जाए, औरों को ज्ञान देने की अपेक्षा स्वयं के ज्ञान को परिपक्व कर लिया जाए, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को ही सुधार लिया जाए, तो अपना भी भला हो सकता है और दूसरे लोगों को भी कर्मजनित प्रेरणा देकर प्रभावित किया जा सकता है। लोग यह कम देखते हैं कि आप कहते क्या हैं? उपदेशक की वार्ता का नहीं, उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव अधिक होता है।
आत्म–ज्ञान की परिपक्वता और गुणों के विकास के लिए आत्म-संबोधन का महत्त्व है। सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन होता रहे, तो मनुष्य अनेक बुराइयों से बचा रह सकता है और आत्म-कल्याण के मार्ग में निष्ठापूर्वक आरूढ़ बना रह सकता है। ईश्वर-भक्ति भी दरअसल आत्म-उद्बोधन का विकसित रूप ही है, जो विचार की अपेक्षा अधिक सरल है। किसी भी विषय को लेकर उसकी गहराई में तन्मय हो जाना और नए-नए तथ्यों की खोज कर लेना सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। कोई थोड़े ही ज्ञानवान, निष्ठावान व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो विचाररत रहकर किन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में विचार आत्म–निर्माण में भी बड़ा सहायक होता है, पर जब किसी के लिए यह स्थिति संभव न हो, तो उसे भावनाओं का आश्रय तो लेना चाहिए। परमात्मा के गुणों का रूप, आकृति, दया-करुणा, उदारता और रक्षा आदि के कार्यों का अपने आप मनन, भजन अथवा कीर्तन करना ही भावना का प्रतीक है। अपेक्षाकृत यह अधिक सरल प्रतिक्रिया है और इस मार्ग द्वारा भी अपने आप को सत्य से उस समय तक जोड़े रखा जा सकता है, जब तक सत्य-सिद्धि न हो जाए अथवा फिर कभी बुराइयों की ओर आकृष्ट हो जाने का भय शेष न रहे।
ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो महत्त्व ईश्वर को उद्बोधन करने का है, आत्म–ज्ञान के मुमुक्षुओं के लिए आत्मा के उद्बोधन का भी वही महत्त्व है। जिस प्रकार भगवान का भक्त यह कहता है—‘‘हे ईश्वर! तू सर्वव्यापक है, विश्व नियंता और सबको धारण करने वाला तू ही है, तूने ही इस सृष्टि की रचना की, आकाश बनाया, समुद्र, पर्वत, नदियां, वृक्ष, फल, फूल और तरह-तरह के जीव बनाए हैं। तू परम दयालु है, पर ममता रहित है, तेरे वश में संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल है, फिर भी तू अहंकार रहित है।’’ इस प्रकार की भावनाएं भक्त की भावनाओं को जीवन प्रदान करती हैं, उसकी ईश्वरनिष्ठा बढ़ती है और वह बुरे विचारों से बचता हुआ, निरंतर कल्याण की ओर अग्रसर होता रहता है।
यह उद्बोधन सच्चे हृदय से आत्मा के लिए किया जाए, तो आत्मा भी अपनी संपूर्ण विशिष्टताएं हम पर प्रकाशित करता है और इस प्रकार आत्म–भावना की पुष्टि भी होती रहती है। ऐसी भावनाएं साधना-काल में, चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते, काम करते हर समय की जा सकती हैं। आत्म-शोधन का यह अनुपम और पूरा मनोवैज्ञानिक तरीका है।
‘‘ऐ आत्मा! तू अपनी ओर देख, तेरी शक्तियों और सामर्थ्यों का क्या ठिकाना? तू अनंत है, महान है, कण-कण में तू ही तो समाया हुआ है। जीव-जंतुओं में, कलरव करते हुए पक्षियों में, लहलहाते हुए खेतों में, महकते हुए फूलों में, धरती-आकाश, जल-थल, सर्वत्र तू ही तू विराजमान है। तेरी ही आत्मा फैल रही है। देख अपने इस विराट स्वरूप को तो देख। इसे देखकर तू आनंद से भर जाएगा।’’
‘‘ऐ जीव! तू शुद्ध और सौंदर्य युक्त है, फिर भी धिक्कार है तुझे, जो इन तुच्छ विषय-भोगों की ओर आकर्षित हो रहा है। उनकी स्थिति क्या है, इस पर कभी विचार किया है? यह तरह-तरह के भोज्य पदार्थ, जिनकी ओर तू ललचाई आंखों से देख रहा है, स्वास्थ्य को गिराने वाले हैं। इन विषय-भोगों के शक्ति-क्षय करने वाले स्वरूप को क्या तू अभी तक नहीं पहचान सका, शरीर की नश्वरता का तूने जरा भी ध्यान नहीं किया, क्या यह तेरे लिए अशोभनीय बात नहीं है?’’
‘‘ऐ जीव! विचार कर कि कितने सौभाग्य से तुझे यह मानव देह उपलब्ध हुई है। तुझे यह भी मालूम नहीं कि तू आया कहां से, कहां जा रहा है? कितना अच्छा होता, यदि तू अपने आप को जानने का प्रयत्न करता और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करता। उदर-पूर्ति तो असहाय पशु-पक्षी भी कर लेते हैं, बच्चे तो ये जानवर भी पैदा कर लेते हैं। आलस्य और निद्रा में मस्त पड़े रहना व समय को व्यर्थ गंवाना तो पशु भी जानते हैं। तू भी इन्हीं सांसारिक क्रिया-कलापों में सीमाबद्ध रहा, तो तेरी विशेषता भी क्या रही? सुख आखिर कब तक रहेंगे? शरीर कब तक साथ देगा? धन कब तक ठहरेगा? ये तो आने-जाने वाले पदार्थ हैं, इन्हें तो तू त्यागपूर्वक ही भोग, आसक्त न हो। आसक्त होने से लाभ भी क्या? तू नहीं तो यह पदार्थ ही एक दिन तुझे छोड़ जाएंगे। विचार कर, शरीर नहीं रहा, तो धन किसके साथ गया? पद, सौंदर्य और सांसारिक सुखों को आज तक कौन अपने साथ ले गया है? इन्हें तू यही तक सीमित रख और शाश्वत स्वरूप को जानने की इच्छा कर।’’
‘‘देख तू माया में, अज्ञान में, अविद्या में, रोगग्रस्त होकर अपने स्वरूप से भ्रष्ट हुआ है। अब तुझे अपने आप को पहचानने की इच्छा हुई है, तो इसे तू अपना महान सौभाग्य ही मान, पर यह और जान ले कि यह कार्य इतना आसान नहीं है, तुझे पग-पग पर कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा, बुराइयों को मारना पड़ेगा और मन की दुष्प्रवृत्तियों को मोड़कर सन्मार्ग की ओर चलना पड़ेगा। पथ दुर्गम है, संघर्ष से भरा है, इनसे लड़ने के लिए तू अपना गांडीव धारण कर अपने पुरुषार्थ का आह्वान कर क्योंकि यह अनंत शक्ति वाला आत्मा केवल साहसी व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाता है। शूरवीर ही इस पथ का अनुसरण कर पाते हैं।’’
इस प्रकार के विचारों का उद्बोधन निरंतर चलते रहना चाहिए। संसार में फैले हुए कलुषित विचारों का मन में प्रभाव न पड़े, ऐसा संभव नहीं। यह आत्मोपदेश बहुत सरल है और उसे हृदयंगम भी किया जा सकता है। प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग भी इसी से संभव है। आत्मा के स्वरूप की प्रतिष्ठा करने से वैसे ही गुणों का विकास होने लगता है। जीवात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने आप को जिस स्थिति का अनुभव करने लगता है, उसकी मनोदशा का झुकाव जिस तरफ हो जाता है, उधर ही उसकी उन्नति होने लगती है और अभ्यास होने पर उस स्थिति की पूर्णता को उपलब्ध कर लेता है।
***
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- आत्म्-सत्ता और उसकी महान महत्ता
- हमारा जीवन लक्ष्य, आत्म-दर्शन
- जीवनोद्देश्य से विमुख न हों
- शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें
- अमर हो तुम, अमरत्व को पहचानो
- मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए
- मनुष्य और उसकी महान शक्ति
- जीवन का दूसरा पहलू भी भूलें नहीं
- आत्मा की पुकार अनसुनी न करें
- आत्मा की पुकार सुनें और उसे सार्थक करें
- आत्म-ज्ञान की आवश्यकता क्यों?
- आत्म-ज्ञान से ही दुःखों की निवृत्ति संभव है
- सत्यं, शिवं सुंदरम्—हमारा परम लक्ष्य
- शक्ति के स्रोत—आत्मा को मानिए
- आत्मा को जानिए
- आत्म-शक्ति का अकूत भंडार
- शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है
- सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे
- चेतन, चित्त—न, चिंतन
- आत्मा और परमात्मा का संबंध
- ईश्वर अंश जीव अविनाशी
- परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो
- अहं और उसकी वास्तविक सत्ता
- बिंदु में सिंधु समाया
- अपूर्णता से पूर्णता की ओर
- क्या आत्—कल्याण के लिए गृहत्याग आवश्यक है?
- आत्म-बल हमारी सबसे बड़ी वैभव-विभूति
- जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ
- आत्म-विकास के लिए व्रत पालन की आवश्यकता