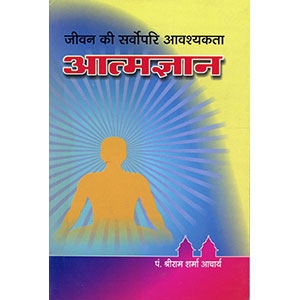जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान 
शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें
इस बात से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव जीवन में शरीर का महत्त्व कम नहीं है। शरीर की सहायता से ही संसार-यात्रा संभव होती है। शरीर द्वारा ही हम उपार्जन करते हैं और उसी के द्वारा सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। यदि मनुष्य को शरीर प्राप्त न हो, तो वह तत्त्व रूप से कुछ भी करने में समर्थ न हो।
यदि एक बार मानव शरीर के इस महत्त्व को गौण भी मान लिया जाए, तब भी शरीर का यह महत्त्व तो प्रमुख है ही कि आत्मा का निवास उसी में होता है। उसे पाने के लिए किए जाने वाले सब प्रयत्न उसी के द्वारा संपादित होते हैं। सारे आध्यात्मिक कर्म जो आत्मा को पाने, उसे विकसित करने और बंधन से मुक्त करने के लिए अपेक्षित होते हैं, शरीर की सहायता से ही संपन्न होते हैं। अतः शरीर का अपरिहार्य महत्त्व है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
शरीर का महत्त्व बहुत है। तथापि, जब इसको आवश्यकता से अधिक महत्त्व दे दिया जाता है, तब यही शरीर जो संसार बंधन से मुक्त होने में हमारी एक मित्र की तरह सहायता करता है, हमारा शत्रु बन जाता है। अधिकार से अधिक शरीर की परवाह करने और उसकी इंद्रियों की सेवा करते रहने से, शरीर और उसके विषयों के सिवाय और कुछ भी याद न रखने से वह हमें हर ओर से विभोर बनाकर अपना दस बना लेता है और दिन-रात अपनी ही सेवा में तत्पर रखने के लिए दबाव में आ जाने वाला व्यक्ति कमाने-खाने और विषयों को भोगने के सिवाय इससे आगे की कोई बात सोच ही नहीं पाता। उसका सारा ध्यान शरीर और उसकी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित हो जाता है। वह शरीर और इंद्रियों की दासता में बंधकर अपनी सारी शक्ति, जिसका उपयोग महत्तर कार्यों में किया जा सकता है, शरीर की सेवा में समाप्त कर देता है। इस प्रकार उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके हृदय में एक पश्चात्ताप रह जाता है, जिसके लिए यह बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य को इस विषय में पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है कि शरीर का कितना महत्त्व है और अपनी सेवा पाने का उसे कितना अधिकार है?
शरीर की सेवा तक सीमित हो जाने की भूल मनुष्य से प्रायः तब होती है, जब वह शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। सत्य बात तो यह है कि मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो साधन मात्र है, साध्य केवल आत्मा ही है, इसलिए प्रधान महत्त्व शरीर को नहीं आत्मा को ही देना चाहिए। आत्मा स्वामी है और शरीर सेवक। इस शरीर को ही आत्मा की सेवा में नियोजित करना चाहिए, न कि आत्मा को शरीर के अधीन कर देना चाहिए। जो इस नियम एवं अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, वे आत्मा की हित-हानि करने वाले भयानक भूल करते हैं, जो निश्चित रूप से शोक, खेद और पश्चात्ताप का विषय है।
शारीरिक स्वार्थ का महत्त्व है लेकर एक सीमा तक। उसी सीमा तक जहां तक वह स्वस्थ, सशक्त और सक्षम बना रहे। वह अशक्यता तथा अल्पायु से बचा रहे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपार्जन करना है और सुख-सुविधा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी। किंतु सच्चा स्वार्थ आत्मा का ही है। उसी की पूर्ति और उसी का हित-साधन करने को प्रधानता दी जानी चाहिए क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य यही है और उसी के लिए यह अनुग्रह भी किया गया है।
शारीरिक स्वार्थ का महत्त्व है लेकर एक सीमा तक। उसी सीमा तक जहां तक वह स्वस्थ, सशक्त और सक्षम बना रहे। वह अशक्यता तथा अल्पायु से बचा रहे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपार्जन करना है और सुख-सुविधा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी। किंतु सच्चा स्वार्थ आत्मा का ही है। उसी की पूर्ति और उसी का हित-साधन करने को प्रधानता दी जानी चाहिए क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य यही है और उसी के लिए यह अनुग्रह भी किया गया है। आवश्यकता से अधिक शरीर की सेवा में लगा रहने से शरीर पुष्ट हो जाता है। उसकी जड़ता प्रबल हो जाती है, आवश्यकताएं वितृष्णा के स्तर पर पहुंच जाती हैं और तब मनुष्य मोह-लोभ-मद-मत्सर आदि ऐसे विकारों से ग्रसित हो जाता है, जो स्पष्टतः आत्मा के शत्रु माने गए हैं। यह विकार अपना अस्तित्व पाकर मानव जीवन को पतन की ओर ही प्रेरित करते हैं, उनका ऐसा करना स्वाभाविक ही है। मनुष्य को पतन की ओर ले जाना विकारों का सहज धर्म है, इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। दोषी तो वास्तव में वह मनुष्य है, जो इनसे अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता। बिच्छू का धर्म है—डंक मारना। यदि वह किसी के डंक मारता है, तो इसके लिए बिच्छू को दोष नहीं दिया जा सकता। दोष तो उस व्यक्ति का ही होगा, जिसने उस कुटिल कीट को कष्ट पहुंचाने का अवसर अपने प्रमाद के कारण दिया। एकमात्र शरीर की सेवा में निरत रहने से उक्त विकार जन्मेंगे, पनपेंगे और अपना अस्तित्व पाकर मनुष्य को धर्मतः पतन की ओर खींचेंगे। अस्तु, अपनी रक्षा के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रधानता शरीर को नहीं आत्मा को दे और उसी के हित-साधन में निरत होकर उसी के कल्याण संपादन का प्रयत्न करे।
शरीर को अपेक्षित अधिकार देकर जो बुद्धिमान व्यक्ति शेष समय तथा रुचियां, आत्मा के स्वार्थ एवं उसकी सेवा करने में लगाते हैं, वे लोक में सुख और परलोक में श्रेय के अधिकारी बनते हैं। शरीर की सेवा जहां मनुष्य को पतन के गर्त में गिराकर रोग-शोक, संताप, पश्चात्ताप आदि की यातना दिलाकर भव-पाशों में लपेटती जाती है, वहां आत्मा की सेवा में मनुष्य अलौकिक सुख, हर्ष-उल्लास, आनंद आदि के साथ मोक्ष एवं मुक्ति का पुरस्कार पाता है। अवश्य ही शरीर की उपेक्षा मत कीजिए। कमाइए, खाइए, गृहस्थी बसाइए, सुख और संपत्ति के अधिकारी बनिए, लेकिन उसमें इस सीमा तक न डूब जाइए कि इसके सिवाय और कुछ सूझ ही न पड़े। शरीर और संसार में उतना ही समय, श्रम और मनोयोग लगाना चाहिए, जितना आवश्यक है और जिससे जीवन की गाड़ी सुविधापूर्वक चलती रहे। शेष का सारा समय, श्रम तथा मनोयोग आत्मा का हित-साधन करने में लगाना चाहिए, जिससे स्वार्थ के साथ परमार्थ और लोक के साथ परलोक भी बनता चले। इसी में जीवन की सार्थकता है।
आत्मिक कल्याण आवश्यक होने के साथ-साथ थोड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए कि मनुष्य प्रायः जन्म-जन्म के संस्कार अपने साथ लाता है। वे संस्कार प्रायः भौतिक अथवा शारीरिक ही होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब मनुष्य का देहाभिमान नष्ट हो जाता है, तो वह मुक्त हो जाता है। उसे शरीर धारण करने की लाचारी नहीं रहती। चूंकि सभी मनुष्यों की अभिव्यक्ति शरीर में हुई, इसलिए यह सिद्ध है कि उसमें अभी शारीरिक संस्कार बने हुए हैं। पूर्व संस्कारों पर विजय पाकर इन्हें आधुनिक रूप में मोड़ लेना, या यो कह लिया जाए कि शारीरिक संस्कारों का आत्मिक संस्कारों से स्थानापन्न कर लेना सहज नहीं होता। संस्कार बड़े प्रबल व शक्तिशाली होते हैं। इन दैहिक संस्कारों को बदलने का सरल-सा उपाय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक कार्यों और शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता की जाती है, उसी प्रकार आत्म-कल्याण की चिंता की जाए। जिस प्रकार सांसारिक सफलताओं के लिए निर्धारित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर प्रयत्न तथा पुरुषार्थ किया जाता है, उसी प्रकार मनोयोगपूर्वक आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाए और प्रयत्नपूर्वक पूरे किए जाते रहें। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने दृष्टिकोण के साथ-साथ पुरुषार्थ की धारा बदल डालें, तो निश्चय ही उसके संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे और वह शरीर की ओर से मुड़कर आत्मा की ओर चल पड़ेगा।
संस्कार बदलने का प्रयत्न करने के साथ-साथ यह भी देखते चलना आवश्यक है कि संस्कारों में अपेक्षित परिवर्तन घटित हो भी रहा है या नहीं। इसकी पहचान यह है कि जब आप देखें कि आत्म-कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता के लिए वैसी ही चिंता रहती है, जैसी कि घर-गृहस्थी के कार्यों और आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने की, तब समझ लें कि संस्कारों में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। यदि भौतिक सफलता की चिंता की तरह आध्यात्मिक सफलता की चिंता नहीं होती, तो समझ लेना चाहिए कि उस दिशा में उचित प्रगति नहीं हो रही है। आप जो कुछ भी आध्यात्मिक प्रयत्न कर रहे हैं, वह सब यों ही एक बेगार अथवा मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। उसमें आपका पूरा-पूरा मानसिक योग नहीं है और आपने उत्तरदायित्व के रूप में उक्त प्रयत्न का मूल्यांकन नहीं किया।
संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए इस प्रकार के हलके-फुलके दिखाऊ प्रयत्न करने से काम न चलेगा, इस कर्तव्य को जीवनलक्ष्य के उत्तरदायित्व की भावना से करना होगा। बहुत से लोग आवेश में आकर जोश-खरोश के साथ संस्कार बदल डालने में सहसा जुट पड़ते हैं। इस प्रकार का असात्त्विक प्रयत्न भी वांछित सफलता संपादित करने में कृतकृत्य न होगा। ज्वार की तरह उठा हुआ कोई भी जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। संस्कारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सात्त्विकी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम अपनाकर और उत्तरदायित्व के साथ उन्हें पूरा करना होगा। प्रगति यदि कम भी है, लेकिन गति में एक दृढ़ता है, तो चिंता की बात नहीं है। कभी-न-कभी वह काम पूरा हो जाएगा। किंतु यदि प्रगति के चरण तो लंबे-चौड़े दीखते हैं और गति में दृढ़ता नहीं है, तो निश्चय ही शीघ्र ही थकान घेर लेगी और उदासीनता गतिहीन हो जाने के लिए विवश कर देगी। संस्कारों में परिवर्तन लाने की योजना तभी सफल होगी, जब स्थिति के अनुसार व्यावहारिक कार्यक्रम बनाया जाए और दृढ़तापूर्वक एक-एक कदम बढ़ाया जाए। ऐसा करने से ही संस्कारों में परिवर्तन संभव है अन्यथा नहीं। जिस दिन अनात्म विषयक कार्यक्रमों की अपेक्षा आध्यात्मिक विषयक अधिक आनंद और उत्साह देने वाले अनुभव होने लगे और शरीर की अपेक्षा आत्मा की चिंता अधिक रहने लगे, तो समझना चाहिए कि संस्कार बदल गए हैं और अब शीघ्र ही हमारा जीवन-यान भवसागर के उस तट की ओर चल पड़ा है, जिस पर कल्याण-कुसुमों से सुशोभित वनस्पति लहलहा रही है।
मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। उसे चाहिए कि वह शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्त्व दे। आत्मा का स्वार्थ ही सच्चा स्वार्थ है जिसे परमार्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। परमार्थ पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि दैहिक संस्कारों के स्थान पर आत्मिक संस्कारों की स्थापना की जाए। इसके लिए आध्यात्मिक कार्यक्रमों को निर्धारित कर उनकी सफलता के लिए चिंतापूर्वक उसी प्रकार प्रयत्न करना होगा, जिस प्रकार भोजन, वस्त्र और घर-गृहस्थी की चिंता की जाती है।
मानव जीवन का लक्ष्य आत्म-कल्याण है। इस लक्ष्य को के लिए आवश्यक है कि आत्मा को शरीर के ऊपर प्रधानता दी जाए। यह क्रिया विचारकोण बदल देने से सहज में पूरी हो सकती है। हम मनुष्य हैं, शरीर ही सब कुछ है। इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार के दैहिक विचारों के स्थान पर इन विचारों को स्थापित करना होगा—हम आत्मा हैं। शरीर तो साधन मात्र है। आत्मा का कल्याण करना ही हमारा परम धर्म है, जिसका निर्वाह हर मूल्य पर करना ही है। इस प्रकार मनुष्य शारीरिक दासता से बचकर आत्मा की सेवा में समर्पित हो जाएगा। जिससे उसे यह पश्चात्ताप करने का अवसर नहीं रहेगा कि ‘‘हाय! मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर अमर आत्मा की उपेक्षा कर दी और अपना सारा जीवन उस शरीर की सेवा में लगा दिया, जो नश्वर है और जिसकी दासता पतनकारी विकार देने के सिवाय और कुछ नहीं दे पाती।’’
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- आत्म्-सत्ता और उसकी महान महत्ता
- हमारा जीवन लक्ष्य, आत्म-दर्शन
- जीवनोद्देश्य से विमुख न हों
- शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें
- अमर हो तुम, अमरत्व को पहचानो
- मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए
- मनुष्य और उसकी महान शक्ति
- जीवन का दूसरा पहलू भी भूलें नहीं
- आत्मा की पुकार अनसुनी न करें
- आत्मा की पुकार सुनें और उसे सार्थक करें
- आत्म-ज्ञान की आवश्यकता क्यों?
- आत्म-ज्ञान से ही दुःखों की निवृत्ति संभव है
- सत्यं, शिवं सुंदरम्—हमारा परम लक्ष्य
- शक्ति के स्रोत—आत्मा को मानिए
- आत्मा को जानिए
- आत्म-शक्ति का अकूत भंडार
- शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है
- सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे
- चेतन, चित्त—न, चिंतन
- आत्मा और परमात्मा का संबंध
- ईश्वर अंश जीव अविनाशी
- परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो
- अहं और उसकी वास्तविक सत्ता
- बिंदु में सिंधु समाया
- अपूर्णता से पूर्णता की ओर
- क्या आत्—कल्याण के लिए गृहत्याग आवश्यक है?
- आत्म-बल हमारी सबसे बड़ी वैभव-विभूति
- जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ
- आत्म-विकास के लिए व्रत पालन की आवश्यकता