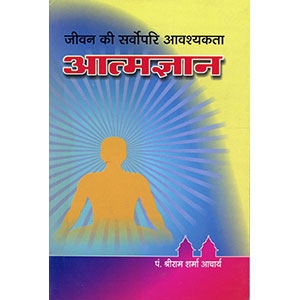जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान 
आत्म-बल हमारी सबसे बड़ी वैभव-विभूति
ईश्वर की कृपा स्वरूप, उनके कृपा और अनुग्रह के रूप में, एक ही पुरस्कार मिलता है—‘आत्म-बल’। यह वह कल्पवृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर हर कामना के समाधान का मार्ग मिल सकता है। यह वह पारस है, जिसको छूकर छोटी परिस्थिति में पड़ा हुआ लोहे जैसा लगने वाला व्यक्ति भी स्वर्ण जैसा शोभायमान और बहुमूल्य बन सकता है। जिसके पास आत्म-बल है, उसके पास कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रह सकती।
गायत्री महामंत्र में सविता देवता के वरेण्यं वर्ण की याचना अथवा उपासना की जाती है। तेजस्वी परमात्मा हमें ब्रह्मतेज प्रदान करेंगे, तो फिर और कमी किस बात की रह जाएगी? स्वर्ण मुद्रा के बदले संसार भर में कहीं भी, कोई भी, वस्तु खरीदी जा सकती है। आत्म–तेज के बदले में भी हर क्षेत्र में प्रगति का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। जिसे यह दैवी वरदान मिल गया, वह धन्य हो गया और जिसे इससे वंचित रहना पड़ा, उसके लिए प्रचुर सुविधा सामग्री होते हुए भी पग-पग पर भय, चिंता, निराशा, आशंका, बेचैनी के दृश्य दृष्टिगोचर होते रहेंगे। उसे कभी चैन की नींद सोने का अवसर न मिलेगा।
अपना स्वरूप, अपना वर्चस्व, अपना महत्त्व न समझने का नाम ही अज्ञान है। बहुत पढ़ा होने पर भी कोई व्यक्ति अज्ञानी ही रहेगा, यदि उसे आत्म-बोध नहीं हुआ। ऐसा अज्ञानी अंधकार में भटकता है और उपनिषद् की भाषा में ‘असुर्या’ नामक तमसाच्छन्न नरक में दुःख-दैन्य की यातना सहता हुआ, रोता-कलपता, जीवन-भार वहन करता है।
यदि हममें आत्मा है—अपने भीतर आत्म-तत्त्व विद्यमान है, तो फिर उसका स्वाभाविक गुण आत्म-बल भी अपने भीतर होना ही चाहिए। उसे कहीं बाहर ढूंढ़ना नहीं पड़ता और न कहीं बाहर से लाना पड़ता है, वह तो अजस्र मात्रा में अपने ही भीतर विद्यमान है। केवल उसे उभारना, निखारना, संभालना भर है। इतने भर प्रयत्न को यदि साधना कहा जाता हो तो उसे कहने, मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। इस साधना का यही स्वरूप है कि हम अपने परम शक्तिशाली स्वरूप की अनुभूति करें और यह समझें कि अपने चारों ओर जो वातावरण घिरा हुआ है, वह मकड़ी के जाले की तरह अपना ही कर्तृत्व है। हमारी भीतरी स्थिति ही बाहरी क्षेत्र में सुख-दुःख अथवा सुविधा-असुविधा का रूप धारण कर घूमती रहती है। हम कारण हैं और परिस्थितियां करण। अपनी मान्यताएं और गतिविधियां ही हैं, जो आरोह-अवरोह बनकर हमें हंसाने-रुलाने के लिए छाया-चित्र की तरह आती-जाती रहती हैं।
हम आज जैसे भी कुछ हैं, अपनी ही मान्यताओं के कारण बने हैं। अपना आंतरिक ढांचा बदल दें, तो बाह्य परिस्थितियों का स्वरूप बदलने में तनिक भी देर न लेगी। भवसागर के बंधन, जंजीरें किसी और ने नहीं बांधी हैं, उन्हें हमने स्वयं ही बनाया और धारण किया है। माया नाम की भवबंधन में बांधने वाली सत्ता का अस्तित्व संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है, उसे अपनी प्रतिगामी मान्यताओं की प्रतिक्रिया मात्र समझना चाहिए।
गुण, कर्म, स्वभाव की दुर्बलताएं ही हमारी प्रगति में मुख्य बाधाएं हैं। यदि अपने में सद्गुणों का, सत्कर्मों का, सत्प्रवृत्तियों का, सद्स्वभाव का बाहुल्य हो, तो निश्चित रूप से संपदाएं और विभूतियां चारों ओर से खिंचकर हमारे आस-पास जमा होने लगेंगी। पुष्प खिलता है, तो उस पर भ्रमर, मधु-मक्खी, तितली अनायास ही मंडराने लगते हैं। मनुष्य का अंतःकरण परिष्कृत हो, व्यक्तित्व उत्कृष्ट बने, तो कोई कारण नहीं कि उसे प्रगतिपथ पर अग्रसर होने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, व्यक्तियों और सूक्ष्म चेतनाओं का सहयोग न मिले। विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों की सफलताओं का मूल कारण यदि बारीकी से तलाश किया जाए, तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि उन्होंने अपने सद्गुणों को बढ़ाया, उनसे गतिविधियां सुव्यवस्थित बनी, इससे दूसरे लोग प्रभावित हुए, उन्हें प्रामाणिक माना। प्रामाणिकता को सहयोग मिलता है। जिसे जनश्रद्धा एवं सहयोग उपलब्ध है, उसके लिए प्रगतिपथ पर आगे बढ़ने के मार्ग में आने वाले अवरोध तृण के समान हैं। वे दीखते भर हैं, सामने आते ही चूर-चूर हो जाते हैं। आत्मा की शक्ति इतनी प्रचंड है कि उसके सामने किसी संकट का ठहर सकना संभव नहीं।
आत्म–बल का प्रकाश ही नगण्य से मानव जीवन को विभूतिवान बनाता है। जीवन की लाश ढोने वाले करोड़ों नर-पशुओं के बीच जो भी अपना अनुकरणीय प्रकरण इतिहास में पृष्ठों पर छोड़ सकने वाले थोड़े से नर-रत्न होते हैं, उनमें दूसरों की अपेक्षा एक ही विशेषता—आत्म-बल की अधिकता होती है। इसके बिना कोई तनकर खड़ा नहीं हो सकता, न कोई महत्त्वपूर्ण निर्माण करता है और न उन महान कार्यों का संपादन करने का साहस कर सकता है, जो मानव जीवन को आनंद और उल्लास से परिपूर्ण प्रकाशवान एवं धन्य बनाते हैं। आत्म-बल ही वह जीवन-तत्त्व है, जो सांस लेते हुए जीवित या मृत के टिड्डी दल में से किसी सजीव को सूर्य-चंद्र की तरह चमकने में समर्थ बना सकता है।
आत्म-बल का रत्न-भंडार आत्म-चेतना की भूमिका में जाग्रत होने पर ही उपलब्ध होता है। ‘मैं आत्मा हूं’ यह मान्यता यदि अंतरात्मा के गहन अंतरंग तक प्रवेश कर जाए, तो व्यक्ति सचमुच यह अनुभव करने लगे कि वह शरीर एवं मन से ऊपर उठी हुई ईश्वरीय पवित्रता एवं महानता से सुसंपन्न आत्मा है। उसे अपनी गतिविधियां आत्मा के कर्तव्य और गौरव के अनुरूप बनानी हैं, तो इस भावना की प्रतिध्वनि उसके रोम-रोम में गूंज उठेगी और नए सिरे से उसे विचार करना होगा कि उसका जीवन लक्ष्य, कर्तव्य एवं गंतव्य मार्ग कहां है? इन प्रश्नों का उत्तर कठिन नहीं है। हर अंतःकरण में इन प्रश्नों का उत्तर मौजूद हैं। उसे किसी गुरु या शास्त्र से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आत्म-चेतना की भूमिका में अंतःकरण जाग पड़े, तो इसे महानतम सौभाग्य कहना चाहिए। ईश्वर का यही सबसे बड़ा अनुग्रह, देवताओं का सबसे बड़ा वरदान और गुरुजनों का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। नर-तन की सार्थकता इस महान जागरण पर ही अवलंबित है। जो इस भूमिका में जगा उसी ने अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को उत्कृष्टता के ढांचे में ढाला और उसी की गतिविधियां आदर्शवादिता का महान प्रकाश बनकर इतिहास के पृष्ठों पर चमकीं। स्वाति बूंद पड़ने से सीप में मोती, केले में कपूर, बांस में वंशलोचन, सर्प में मणि उत्पन्न होने की बात सुनी गई है।
ये बातें प्रामाणिक हों चाहे अप्रामाणिक, पर यह नितांत सत्य है कि आत्म-चेतना की भूमिका में जगा हुआ मनुष्य नर से नारायण बन जाता है। पपीहे की प्यास स्वाति नक्षत्र का जल पीने से शांत होती सुनी गई है, कह नहीं सकते कि यह कहां तक ठीक है, पर यह नितांत सत्य है कि आत्मा की प्यास तभी बुझती है, जब अंतःकरण आत्म-चेतना की भूमिका में जाग जाता है और यह अनुभव करता है कि मैं शरीर और मन नहीं, वरन् अविनाशी आत्मा हूं। मुझे शरीर और मन की लपक बुझाते रहने के लिए नहीं, वरन् आत्मा के गौरव की कथा कहने के लिए इस बहुमूल्य मानव जीवन के एक-एक क्षण का सदुपयोग करना है।
इस धर्म संकट की घड़ी में आत्मा को महाभारत के अर्जुन की स्थिति में खड़ा होना होता है। चिर परिचित, चिर अभ्यस्त पुरानी मान्यताएं एवं गतिविधियों के प्रति मोह, ममता का होना स्वाभाविक है। अर्जुन अपने चारों ओर स्वजन, संबंधियों से घिरा हुआ और खड़ा हुआ देखता है। वे सभी विरोधी बने हुए हैं। इनसे कैसे लड़ा जाए? यह मोह अर्जुन को आ घेरता है और वह गांडीव को नीचे रखकर बैठ जाता है। आत्म-भूमिका में जाग्रत हुआ व्यक्ति अपनी वर्तमान गतिविधियों पर दृष्टि डालता है, तो वे निरर्थक बाल-क्रीड़ा मात्र दीखती हैं। जरा-सा पेट, थोड़े-से परिश्रम से गुजर की संभावना फिर अधिकाधिक धन कमाने के पीछे जीवनलक्ष्य के लिए अनावश्यक कर्तव्यों की उपेक्षा क्यों? कुत्ते द्वारा सूखी हड्डी चबाते जाने पर अपने ही जबड़ों का रक्त पीकर उसे जो प्रसन्नता होती है, वैसा ही अनुकरण इंद्रिय-वासना के लिए जीवन-तत्त्व को निचोड़ते हुए करते रहने में क्या बुद्धिमत्ता है?
अनेक दोष-दुर्गुणों और अवांछनीय क्रिया-कलापों में संलग्न जीवनक्रम से इतना मोह किसलिए? ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कर्तव्य कहता है, पुराने ढर्रे को तोड़ो, इससे लड़ो और अवांछनीय को हटाओ, पर अर्जुन का मोह उस पुराने, चिर अभ्यास, चिर-परिचित ढर्रे को छोड़ने, तोड़ने का साहस नहीं कर पाता और सोचता है जैसा चह रहा है, वैसा ही चलने दिया जाए। कर्तव्यपालन यदि इतना झंझट भरा है—आत्म-जागरण का यदि इतना महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है, तो उसे छोड़ ही क्यों न दिया जाए।
गीता ग्रंथ आत्मा की इसी समस्या को सुलझाने के लिए लिखा गया है। भगवान् ने अनेक तर्कों और तथ्यों के आधार पर अर्जुन को समझाया कि—‘‘यह चिर-परिचित गतिविधियां कुटुंबी, संबंधियों की तरह अति निकटवर्ती और प्रिय बन गई हैं, फिर भी इन्हें हटाया जाना आवश्यक है। यदि इन्हें जहां-के-तहां यथावत रहने दिया गया, तो अनीति और पाप का ही दौर-दौरा बना रहेगा। साधना-समर में अपने ही अज्ञान असुर से तो लड़ना पड़ता है, यदि इस संघर्ष-संग्राम से इनकार किया गया, तो वीर क्षत्रियों को मिलने वाले श्रेय और स्वर्ग से वंचित रहना पड़ेगा। कर्तव्य धर्म के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है। यदि संघर्ष से मुख मोड़ना है, तो कर्तव्य धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। अतएव हे अर्जुन, चिर-परिचितों का चिर-सहचरों का मोह छोड़ और वह कर जिसमें श्रेयस की साधना संपन्न होती है।’’
आत्म–बल उपलब्ध करने की साधना करने वाले हर साधक को अर्जुन का अनुसरण करते हुए अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना होता है। उसे सबसे पहला काम आत्म-निरीक्षण द्वारा अपनी दुष्प्रवृत्तियों और मूर्खताओं का निराकरण करना होता है। जो गतिविधियां शरीर और मन को प्रसन्नता दें, पर आत्मा को भूखा मारें, उन्हें मूर्खता नहीं, तो और क्या कहा जाए? जो प्रवृत्तियां नश्वर संसार की विनोदात्मक हलचलों में रस लेने के लिए प्रेरित करती रहें, उसके लिए कुकर्म करने तक के लिए फुसलावे और आत्मा को नारकीय यातनाएं सहने को विवश करें, उन्हें मूर्खता नहीं तो और क्या कहें? विवेक भूमिका में जाग्रत आत्मा यदि अपनी मूर्खताओं को भी न हटा सका, तो उसके जागरण का आखिर प्रयोजन ही क्या रहा?
आत्म–बल वे उपार्जित करते हैं, जो आत्म-समीक्षा और आत्म-सुधार के लिए अपनी चिर अभ्यस्त गतिविधियों को उलट-पुलट डालने का साहस कर सकें और मार्ग में जो उपहास, विरोध, कष्ट एवं अवरोध सहना पड़े, उसे धैर्यपूर्वक सहन कर लें। भौतिक एवं आत्मिक प्रगति के लिए, संपत्तियों और विभूतियों से सुसंपन्न बनने के लिए, आत्म-बल आवश्यक है। उसकी उपयोगिता हमें जाननी ही चाहिए और संसार के इस एकमात्र सारतत्त्व को प्राप्त करने के लिए कुछ उठा न रखना चाहिए। संसार के सारे वैभव आत्म-बल की तुलना में तुच्छ हैं। जिसके पास आत्म-बल है, वही आत्म भूमिका में जाग्रत हुआ जीवनयुक्त नर-नारायण है। जो आत्म–बल संपन्न है, उसके लिए इस संसार में ऐसा कुछ नहीं, जिसे असंभव कहा जा सके।
***
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- आत्म्-सत्ता और उसकी महान महत्ता
- हमारा जीवन लक्ष्य, आत्म-दर्शन
- जीवनोद्देश्य से विमुख न हों
- शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें
- अमर हो तुम, अमरत्व को पहचानो
- मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए
- मनुष्य और उसकी महान शक्ति
- जीवन का दूसरा पहलू भी भूलें नहीं
- आत्मा की पुकार अनसुनी न करें
- आत्मा की पुकार सुनें और उसे सार्थक करें
- आत्म-ज्ञान की आवश्यकता क्यों?
- आत्म-ज्ञान से ही दुःखों की निवृत्ति संभव है
- सत्यं, शिवं सुंदरम्—हमारा परम लक्ष्य
- शक्ति के स्रोत—आत्मा को मानिए
- आत्मा को जानिए
- आत्म-शक्ति का अकूत भंडार
- शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है
- सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे
- चेतन, चित्त—न, चिंतन
- आत्मा और परमात्मा का संबंध
- ईश्वर अंश जीव अविनाशी
- परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो
- अहं और उसकी वास्तविक सत्ता
- बिंदु में सिंधु समाया
- अपूर्णता से पूर्णता की ओर
- क्या आत्—कल्याण के लिए गृहत्याग आवश्यक है?
- आत्म-बल हमारी सबसे बड़ी वैभव-विभूति
- जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ
- आत्म-विकास के लिए व्रत पालन की आवश्यकता