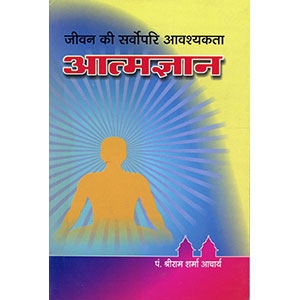जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान 
अहं और उसकी वास्तविक सत्ता
छांदोग्योपनिषद् में एक कथा आती है। एक बाद इंद्र और विरोचन दो व्यक्तियों में अपने आपको जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। ‘मैं क्या हूं?’ वे बार-बार इस पर सोचते-विचारते, लेकिन उन्हें ‘‘मैं’’ का अता-पता नहीं लगा। आखिर दोनों मिलकर आदरपूर्वक शिष्य भाव से हाथ में समिधाएं लेकर आचार्य प्रजापति के पास गए और नम्रतापूर्वक उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उनके प्रश्न का जवाब देते इसके पूर्व ही प्रजापति ने उनकी योग्यता, पात्रता को जानने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा—‘‘थाली में पानी भरकर अपना-अपना मुंह देखो, उसमें तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई देगा।’’
इंद्र और विरोचन दोनों झट से सज धजकर पानी से भरी थाली में अपने को देखने लगे। विरोचन को अपना सजा-संवारा रूप देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने साथियों में जाकर अभिमान के साथ कहने लगा—‘‘भाई, मैंने तो, ‘मैं’ का पता लगा लिया है।’’ इंद्र कुछ बुद्धिमान था, उसे संतोष नहीं हुआ और वह आचार्य प्रजापति के पास जाकर कहने लगा—‘‘भगवान! असंस्कृत शरीर की प्रतिच्छाया ही प्रतिबिंब में दिखाई देती है। यदि यह शरीर काना, लूला, लंगड़ा होता तो प्रतिच्छाया भी वैसी ही दिखाई देती, वस्त्र-अलंकारों को उतार देने पर प्रतिबिंब का सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर यह भी नहीं रहता। इसलिए मैं अपना स्वरूप किसे मानूं? मुझे इससे शांति नहीं मिलती।’’
—छांदोग्योपनिषद् 8/92
इंद्र समझदार था। सोचा इन वस्त्र-अलंकारों से सजा हुआ शरीर ही यदि ‘‘मैं हूं’’, तो यह निश्चित है कि इनके नष्ट होते ही मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। इनके मैले, जीर्ण-शीर्ण होने पर ‘‘मैं’’ भी त्याज्य बन जाऊंगा। जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, वह कदापि ‘‘मैं’’ नहीं हो सकती और इंद्र को इससे शांति नहीं हुई और न ही उसको समाधान ही मिला। अपने इस मनोभाव को उसने आचार्य के समक्ष निर्भय होकर प्रकट कर दिया। उधर विरोचन अपने सजे हुए सुंदर वस्त्र-अलंकारों से विभूषित शरीर के प्रतिबिंब को ही ‘‘मैं’ का स्वरूप जानकर के चला गया।
हम में से बहुत कम लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है ‘‘मैं क्या हूं?’’ इस पर बहुत कम लोग ही सोचने-विचारने का प्रयत्न करते हैं। अधिकांश तो भवसागर के प्रवाह में बहने वाले ही बनकर रहते हैं। उनके मन, बुद्धि, चेतना पर अज्ञान का परदा इस तरह पड़ा रहता है कि वे कभी यह सोचते तक नहीं कि वे कौन हैं? उन्हें क्या करना है? कहां जाना है?
कुछ लोग मैं के अस्तित्व को शरीर तक ही मानकर विरोचन की-सी भूल कर बैठते हैं और शरीर को सुख देने, खाने-पीने, खुश रहने, मौज-मजा उड़ा लेने में ही जीवन का सार समझते हैं। लेकिन यदि शरीर को ही मैं का स्वरूप मान लिया जाए, तो फिर जीवन का मूल्य ही क्या रह जाता है। कोई झंझट ही फिर शेष नहीं रह जाता। कुछ करने या न करने का कोई महत्त्व नहीं रहता, फिर ज्ञान-विज्ञान की बात कौन करे? फिर न जीने से लाभ रहता, न मरने से हानि, क्योंकि सभी शरीरों की एक ही गति होती है। किसी-न-किसी समय में वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी-अज्ञानी, सत्यवादी और झूठा, सज्जन एवं दुर्जन सभी को तो शरीर की दृष्टि से एक दिन मिट जाना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में तो मरने से पहले का कोई महत्त्व नहीं, तो मरने के बाद में कोई अस्तित्व नहीं रहता। जीवन सिर्फ दो अंधकार के बीच की पतली-सी रेखा मात्र है। देर-अबेर में फट जाने वाले, मैले पड़ जाने वाले वस्त्रों का-सा मूल्य है, हमारे जीवन का, चाहे वह सादा हो या चमकदार। लेकिन क्या हमें इतना सोच लेने पर से इंद्र की तरह असंतोष नहीं होता? ‘‘मैं’’ को जानने की जिज्ञासा कर इससे समाधान नहीं हो रहा, ऐसा महसूस होने लगता है हमें।
फट जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले वस्त्राभूषणों से युक्त प्रतिबिंब को ‘‘मैं’’ का स्वरूप जान लेने से हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती। क्योंकि इन्हें धारण करके हम अच्छे लगते हैं और उतार फेंकने पर कुरूप। इस तरह स्पष्ट है कि वस्त्र-आभूषण ‘‘मैं’’ का परिचय नहीं हो सकते। अपना वस्त्र फट जाने पर यह आभास नहीं होता कि मैं फट गया। वस्त्र-आभूषण उतार देने या पहने रहने पर ‘‘मैं’’ का अस्तित्व बना ही रहता है।
ठीक यही स्थिति शरीर के साथ भी है। वस्त्रों की तरह हमारा शरीर नित्य ही किसी-न-किसी रूप में नष्ट होता रहता है। मल, शरीर से निकलने वाले दूषित तत्त्व—क्या हैं? नष्ट हुए शरीर का अवशेष। रसायनशास्त्री वैज्ञानिकों के प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर में नित्य असंख्यों कोश नष्ट होते हैं, असंख्यों ही नए पैदा होते हैं, इस तरह शरीर की दृष्टि से तो हम नित्य ही मरते हैं और नित्य ही जन्म लेते हैं। लेकिन ‘‘मैं’’ के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता।
इसी तरह शरीर का कोई अंग कट जाने पर कोई यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि उसका ‘‘मैं’’ कट गया। उंगली कट जाने पर, आंख फूट जाने पर यह तो मालूम होता है कि मेरे शरीर में कुछ क्षति हो गई है। लेकिन हमें यह विश्वास नहीं होता कि हम अपूर्ण हो गए। अपनी अज्ञान पूर्णता के अस्तित्व में हमारी सहज आस्था कम नहीं होती। ‘‘मैं हूं’’—यह भावना कभी नष्ट नहीं होती।
‘‘मैं’’ की खोज में हम आगे बढ़ें, इससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर ‘‘मैं’’ को जान लेने की आवश्यकता क्यों है? बहुत-से लोग तो इस संबंध में कुछ सोचते-विचारते नहीं। ऐसे लोगों को खाने-पीने, मौज उड़ाने से फुरसत नहीं मिलती, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति पशुत्व की द्योतक है। क्योंकि शायद ही पशुओं के मन में अपने भूत-भविष्य के बारे में सोच-विचार करने की तरंग उठती हो। उनको अपने प्रकृति-प्रेरित कार्यों में लगे रहना ही प्रिय होता है।
कुछ बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग इस महा प्रश्न में बेकार न लगकर अपना काम करना ही अधिक अच्छा समझते हैं। वे इस जटिल प्रश्न को सुलझाने में व्यर्थ श्रम करना अच्छा नहीं समझते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? यह निश्चय करना इससे भी कठिन है और बिना सही निश्चय के किए गए कार्य अंततः मनुष्य के लिए अशांति, असंतोष के कारण ही बनते हैं। कर्तव्य का निश्चय भी तभी हो सकता है, जब हम अपने असली अस्तित्व का जानकारी का सकें। यदि हम शरीर ही हैं, तो फिर हमारे कर्तव्यों की सीमा भी शरीर तक ही सीमित रहेगी। किसी भी कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय हमें वहीं तक करना होगा, जितना इसी जीवन से संबंध है। उदाहरणार्थ हमें किसी जगह एक माह रहना है, तो वहां वर्षों में बनने वाले भव्य भवन बनाने की योजनाएं किस काम की? इसी तरह मैं, का अस्तित्व यदि शरीर से परे महान है, लंबा है, तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्णय भी इसी आधार पर करना पड़ेगा।
तात्पर्य यह है कि अपने आप को जाने बिना जीवनपथ पर, कर्तव्य मार्ग पर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अभाव में तो हमारी स्थिति ठीक वैसी होगी, जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद किए जंगल में तेजी से दौड़ रहा हो। उससे पूछा जाए, ‘‘भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम्हें कहां जाना है, कहां से आए हो?’’ और इसका उत्तर वह अपनी अजानकारी में दे, तो हम उसे पागल ही कहेंगे। क्या हमारी स्थिति भी अपने स्वरूप को जाने बिना कुछ ऐसी ही नहीं है? इसलिए ‘मैं’ के स्वरूप की जानकारी करना, इस संबंध में प्रारंभिक आधार खोजकर आगे बढ़ना नितांत आवश्यक है। इसके बिना हम अपने जीवन की सही रूपरेखा न बना सकेंगे, न अपने कर्तव्यों का, अपनी गति की दिशा का सही-सही निर्धारण ही कर सकेंगे। अपने स्वरूप को जानना जीवन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
सचमुच जीवन का वास्तविक लाभ वे ही उठा पाते हैं, जो पहले अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं। अपने को न जानने वाले व्यक्ति तो उन आधारहीन वस्तुओं की तरह हैं, जिन्हें वायु का झोंका, किधर भी बहाकर ले जा सकता है। ऐसे लोगों को संसार-प्रवाह में बलात् बहते रहना पड़ता है।
***
Write Your Comments Here:
- दो शब्द
- आत्म्-सत्ता और उसकी महान महत्ता
- हमारा जीवन लक्ष्य, आत्म-दर्शन
- जीवनोद्देश्य से विमुख न हों
- शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें
- अमर हो तुम, अमरत्व को पहचानो
- मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए
- मनुष्य और उसकी महान शक्ति
- जीवन का दूसरा पहलू भी भूलें नहीं
- आत्मा की पुकार अनसुनी न करें
- आत्मा की पुकार सुनें और उसे सार्थक करें
- आत्म-ज्ञान की आवश्यकता क्यों?
- आत्म-ज्ञान से ही दुःखों की निवृत्ति संभव है
- सत्यं, शिवं सुंदरम्—हमारा परम लक्ष्य
- शक्ति के स्रोत—आत्मा को मानिए
- आत्मा को जानिए
- आत्म-शक्ति का अकूत भंडार
- शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है
- सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे
- चेतन, चित्त—न, चिंतन
- आत्मा और परमात्मा का संबंध
- ईश्वर अंश जीव अविनाशी
- परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो
- अहं और उसकी वास्तविक सत्ता
- बिंदु में सिंधु समाया
- अपूर्णता से पूर्णता की ओर
- क्या आत्—कल्याण के लिए गृहत्याग आवश्यक है?
- आत्म-बल हमारी सबसे बड़ी वैभव-विभूति
- जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ
- आत्म-विकास के लिए व्रत पालन की आवश्यकता