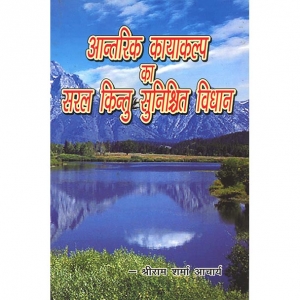आन्तरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिश्चित विधान 
प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
Read Scan Versionचान्द्रायण साधना का पूर्वार्द्ध है—पश्चात्ताप और उत्तरार्ध है क्षति पूर्ति। दोनों को मिला देने पर ही प्रायश्चित की वह समग्र प्रक्रिया पूर्ण होती है जिसके आधार पर इस जनम के एवं पूर्व जन्मों के संचित क्रियमाण दुष्कृत्यों का निराकरण होता है। उपवास भी उस चतुर्विध तपश्चर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर इतने भर से ही समग्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जीवन निर्वाह में भोज महत्वपूर्ण तो है, पर उसके अतिरिक्त भी जल, सांस तथा विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। उपवास को भोजन माना जाय तो चान्द्रायण के साथ जुड़े हुए अन्य अंग-अनुशासनों को भी कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
मनुष्य के किए हुए दुष्कर्म ही सांसारिक सुख और आत्मिक प्रगति में प्रमुख बाधा बनकर खड़े रहते हैं। पैर में कांटा लग जाने पर सारे शरीर को कष्ट होता है और नींद नहीं आती। जब तक उसे निकाल बाहर न किया जाय तब तक चैन नहीं पड़ता। विषैला पदार्थ खा लेने पर पेट में जलन होती है, भारी कष्ट होता है और मृत्यु संकट सामने आ खड़ा होता है। वमन-विरेचन द्वारा उसे विभिन्न नाच नाचने, क्रिड़ा कौतुक करने के लिए विवश करती रहती है। इतना ही नहीं वह परिस्थितियां भी इतनी जटिल उत्पन्न कर देती है जो टाले नहीं टलती। कारण कि इनकी जड़ें अचेतन की गहन परतों में होती हैं। जड़ न कटे तो टहनी तोड़ने से ही वृक्ष के अस्तित्व पर क्या असर पड़ने वाला है।
इन दिनों शारीरिक रोगों की अभिवृद्धि दिन दूनी, रात चौगुनी होती जा रही है। चिकित्सकों, चिकित्सालयों एवं नित नई औषधियों में आंधी तूफान की तरह बढ़ोत्तरी हो रही है, इतने पर भी उसके नियंत्रण के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। इस असमंजस का समाधान एक ही है कि मनःक्षेत्र में घुसती-पनपती उन कुत्साओं-कुण्ठाओं का पर्यवेक्षण निराकरण किया जाय जो न केवल शारीरिक रोगों-मानसिक उद्वेगों के लिए जिम्मेदार हैं, वरन् व्यावहारिक जीवन में भी अनेकानेक विग्रह संकट आये खड़े करती है। मनःस्थिति परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है इस तथ्य को समझ लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव हो सकेगा कि संकटों का आत्यन्तिक समाधान क्या हो सकता है?
मनोविज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि शारीरिक रोगों का प्रमुख कारण मनःक्षेत्र में जमे हुए हठीले कुसंस्कार ही होते हैं—हठीले इस अर्थ में कि उन्हें धारण किया हुआ व्यक्ति यह भली-भांति समझता है कि उसने जो अनुपयुक्तताएं अपना रखी हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। इतने पर भी वे स्वभाव के साथ बुरी तरह गुंथ गईं, आदतों के रूप में इस प्रकार परिपक्व बन गई होती हैं कि उन्हें हटाने के सामान्य उपायों से कोई ठोस परिणाम निकलता दिखाई नहीं पड़ता। समझदारी का तकाजा एक ओर, आदतों का हठीलापन दूसरी ओर। यदि इन दोनों की तुलना की जाय तो कुसंस्कारों का हठीलापन ही भारी पड़ता है।
सभी जानते हैं कि मनुष्य ही है जो मानसिक असंतुलन उत्पन्न करता है और उनके विक्षोभों के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अवयवों की सामान्य कार्य पद्धति में अवरोध उत्पन्न करता है। फलतः बीमारियां उसे आ घेरती हैं।
शरीर यात्रा में रक्त संचार का कितना ही महत्व क्यों न हो वस्तुतः उसका नियंत्रण केन्द्र मस्तिष्क में रहता है। हृदय पोषण देता है यह सही है, उसमें प्रोत्साहन एवं नियमन की क्षमता नहीं, यह कार्य मस्तिष्क का है। उसी के ज्ञान तन्तु मेरुदण्ड के माध्यम से समस्त शरीर में फैलते हैं और निर्देश देकर सारे काम कराते हैं। मस्तिष्क में नींद आने लगे तो अंग-अंग सहज ही शिथिल होते चले जाते हैं। आकुंचन-प्रकुंचन, निमेष-उन्मेष, श्वास-प्रश्वास क्रियायें अचेतन-संस्थान के इशारे पर चलती हैं। जीवनी शक्ति भोजन से नहीं वरन् मनोगत साहसिकता और प्रसन्नता के आधार पर मिलती और पनपती है। यदि इस केन्द्र में गड़बड़ी चले तो उसका प्रभाव शरीर के विभिन्न अवयवों पर पड़े बिना रह नहीं सकता।
रोगों की जड़ शरीर में हो; तो काय चिकित्सा से सहज सुधार होना चाहिए। पोषण की पूर्ति आहार से होनी चाहिए और विषाणुओं को औषधि के आधार पर हटाने में सफलता मिलनी चाहिए। किन्तु देखा जाता है कि जीर्ण रोगियों की काया में रोग बुरी तरह रम जाते हैं कि उपचारों की पूरी पूरी व्यवस्था करने पर भी हटने का नाम नहीं लेते। एक के बाद दूसरे चिकित्सक के नुस्खे बदलते रहने पर भी रुग्णता से पीछा नहीं छूटता। इलाज के दबाव में बीमारियां रूप रंग बदलती रहती हैं, वा जड़ें न कटने से टूटे हुए वृक्ष फिर से नई कोपलों की तरह उगते हैं। जड़ों को खुराक मिलती रहे तो टहनियां तोड़ने से भी पेड़ सूखता नहीं है।
रोगों के दो वर्ग हैं एक आधि दूसरा व्याधि। व्याधि शारीरिक रोगों को और आधि मानसिक रोगों को कहते हैं। ज्वर, खांसी, दमा, दर्द, अपच, मधुमेह, रक्तचाप आदि को शारीरिक रोग में गिना जाता है और उन्माद, सनक, मूर्खता, विस्मृति, विसंगतियां, उलझन आदि की मानसिक रोगों में गणना होती है। मस्तिष्कीय रोगों की चिकित्सा पागलखाने के डॉक्टर करते है और मनःचिकित्सक पूछताछ करके अंतरंग में जमी कुण्ठाओं को उगलवाने और सत्परामर्श देने के उपायों का सहारा लेते हैं। शरीर विज्ञानी उपचार औषध शल्य कर्म आदि के द्वारा करते हैं। इनमें आंशिक सफलता भी मिलती है, पर प्रयत्न फिर भी अधूरा ही रह जाता है। वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा अभीष्ट है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए मन की उस गहराई तक जाना होगा जहां से कि शरीर और मन को प्रभावित करने वाले प्रवाहों को उभारने और काम करने की प्रेरणा मिलती है। कुंए में जो पानी भरा दीखता है वह उसकी तली में जल फेंकने वाले स्रोतों से आता है। इसी प्रकार मस्तिष्कीय अस्त-व्यस्ततायें चेतना की मूल प्रवृत्ति के मर्मस्थल में से उभरती हैं। मनुष्य के गहन अन्तराल में कुछ आस्थायें जैसी होती हैं। व्यक्तित्व का मूल स्रोत उन्हीं में सन्निहित है।
पौराणिक प्रतिपादन है कि देवता स्वर्ग में ऊर्ध्वलोक में रहते हैं और दानव भूमि से नीचे पाताल में—पतितावस्था में रहते हैं। देवताओं का स्वर्ग लोक आकाश में ऊंचाई पर है। इन्हें उत्कृष्टता और निकृष्टता का लोक कह सकते हैं। लोकों का वर्णन किया गया तो इस प्रकार है मानो ये कोई देश क्षेत्र हों, पर वस्तुतः वे मनोभूमियों पर हैं और उन्हें दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। स्वर्ग में सुख-सम्पदायें भरी पड़ी हैं और नरक में यातनाएं ही यातनाएं हैं। यह यातनाएं मरने के बाद ही मिलती हों ऐसी बात नहीं है। उनका अनुभव इसी जीवन में, इसी शरीर में भी किया जाता है। शारीरिक व्याधियां और मानसिक आधियों को इसी रूप में लिया जा सकता है।
अन्तःकरण की आस्थाएं ही हैं जो मनुष्य को ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की प्रेरणा देती हैं। उसी की प्रतिक्रिया व्यक्तित्व को समुन्नत एवं पतित बनाकर रख देती हैं। इसी आन्तरिक उत्थान-पतन के आधार पर मनुष्य स्वर्गीय एवं नारकीय दृष्टिकोण विनिर्मित करता है और तदनुसार अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक कष्टों को सहन करना पड़ता है। इतना ही नहीं जीवन के अन्य क्षेत्र भी ऐसी विषम परिस्थितियों से भर जाते हैं जिनमें रहने वाला अपने को पग-पग पर असफल, उपेक्षित, तिरस्कृत, दरिद्र और दुर्भाग्यग्रस्त अनुभव करता है।
डॉ. ब्राउन, डॉ. पीले मैगडूगल, हेडफील्ड और डॉ. जुंग आदि अनेक प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्रियों ने यह माना है कि फोड़े-फुन्सी से लेकर टी.बी. और कैंसर तक की बीमारियों के पीछे कोई दूषित संस्कार ही कारण होते हैं। मनुष्य बाहर से ईश्वर परायण, सत्यभाषी, मधुर-व्यवहार करने वाला दिखाई देता है। पर सच बात यह होती है कि यदि अन्तर्मन की नैतिकता को दबाकर केवल दिखावे के लिए कुछ किया जाता है तो उसका मन भीतर ही भीतर अन्तर्द्वन्द्व करता है। उस अर्न्तद्वन्द्व के फलस्वरूप ही उसमें रोग पैदा होते हैं। कई बार यह संस्कार बहुत पुराने हो जाते हैं, तब बीमारी फूटती है। पर यह निश्चय है कि बीमारियों का पदार्पण बाहर से नहीं व्यक्ति के मन से ही होता है।
इस कथन की पुष्टि में श्री मैक्डोनल्ड अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं—‘अमेरिका के बीमारों में आधे ऐसे होते हैं, जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, क्रोध, धोखे-बाजी आदि भाव प्रभुत्व जमाये होते हैं। जो इस प्रकार मानसिक रोगी होते हैं, वे अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं कर सकते, उनका व्यक्तित्व अस्त-व्यस्त हो जाता है, उसी से वे उल्टे काम करते और बीमारियों को बढ़ाते हैं।’ आगे दुश्चिन्ता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए श्री मैकडोनल्ड लिखते हैं—‘‘मानसिक चिन्ताओं द्वारा रक्त के अन्दर ‘एड्रेनलीन’ नामक हारमोन की अधिकता हो जाती है, उसी से श्वास फूलना, कम्पन, चक्कर आना, बेचैनी, दिल धड़कना, पसीना आना और दुःस्वप्न बनते हैं। दौरे और बड़ी बीमारियां भी किसी न किसी मानसिक ग्रन्थि के ही परिणाम हो सकते हैं, जिसे डॉक्टर नहीं जानता, कई बार मनुष्य भी नहीं जानता, पर व्याधियां होतीं मन का कुचक्र ही है।’’
इस सम्बन्ध में भारतीय मत बहुत स्पष्ट है। यहां जीवन को इतनी गहराई से देखा गया है कि आधि-व्याधि के मानसिक कारण पाप-ताप के संस्कार रूप में स्पष्ट झलकने लगते हैं। योग-वाशिष्ठ में ऋषि कहते हैं—
यित्ते विधुरते देहः संक्षोभमनुयात्यलम् ।
— 6।1।81।30
चित्त में गड़बड़ होने से शरीर में गड़बड़ होती है।
इदं प्राप्तमिदं नेयि जाड्याद्धा घनमोहदाः ।
आधयः सम्प्रवर्तन्ते वर्षासु मिहिका इव ।।
— 6।1।81।16
अन्तर्द्वन्द्व और अज्ञान से मोह में डालने वाले मानसिक रोग पैदा होते हैं, फिर शारीरिक रोग इस तरह पैदा हो जाते हैं, जैसे बरसार के दिनों में मेंढक अनायास दिखाई देने लगते हैं।
दुष्काल व्यवहारेण दुष्क्रिया स्फुरणेन च ।
दुर्जना संगदोषेण दुर्भावोद्भावनेन च ।
क्षीणत्वाद्वा प्रपूणत्वन्नाडीनां रन्ध्रसन्ततौ ।
प्राणे विधुरतां याते काये तु विकलीकृते ।
—6।1।81।18।19
दौस्थित्यकारणं दोषाद्धयाधिर्देहे प्रवर्तते ।
अनुचित समय पर अनुचित काम करने से, बुरे लोगों के पास बैठने से मनुष्य मन में पाप और बुरी भावनाओं को स्थान देने लगता है। ऐसा होने पर नाड़ियां अपनी सामान्य कार्य-प्रणाली बंद कर देती है। कुछ नाड़ियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, कुछ अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, जिससे प्राण का बहाव उलटा-पुलटा हो जाता है। प्राण संचार में गतिरोध उत्पन्न होने पर ही शरीर की स्थिति बिगड़ती और उसमें तरह-तरह के रोग पैदा हो जाते हैं।
आगे चलकर योग वाशिष्ठ ग्रन्थ में इस प्रसंग का और भी अच्छी तरह खुलासा किया गया है—
संक्षोभात्साम्युत्सर्ज्य वहन्ति प्राणवायवः ।
—6।1।81।32
असमं बहति प्राणे नाड्योयन्ति विसंस्थितिम् ।
—6।1।81।33
काश्चिन्नाड्यः प्रपूर्णत्वं यान्तिकाश्चिच्चरिक्तताम् ।
—6।1।81।34
कुजीर्णत्वमजीर्णत्व मतिजीर्णत्वमेव वा ।
दोषा यैव प्रपात्यन्नं प्राणसंचारदुष्क्रमात् ।।
—6।1।81।35
तथान्नानि नत्यन्तः प्राणवातः स्वामाश्रयम् ।
—6।1।81।36
यान्यन्ननि निरोधेन तिष्ठन्त्यन्तः शरीर के ।
—6।1।81।37
तान्येव व्याधितां यान्ति परिणामस्वभावतः ।
—6।1।81।38
एवमाघेर्मवेव्द्याधिस्तस्याभावाच्च नश्यति ।।
—6।1।81।31
अर्थात् चित्त में उत्पन्न हुए विकार से ही शरीर में दोष पैदा होते हैं। शरीर में क्षोभ या दोष उत्पन्न होने से प्राणों के प्रसार में विषमता आती है और प्राणों की गति में विकार होने से नाड़ियों के परस्पर सम्बन्धों में खराबी आ जाती है। कुछ नाड़ियों की शक्ति का तो स्राव हो जाता है, कुछ में जमाव हो जाता है।
प्राणों की गति में खराबी से अन्न अच्छी तरह नहीं पचता। कभी कम कभी अधिक पचता है। शरीर के सूक्ष्म यंत्रों में अन्न के स्थूल कण पहुंच जाते और जमा होकर सड़ने लगते हैं, उसी से रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आधि (मानसिक रोग) से ही व्याधि (शारीरिक रोग) उत्पन्न होते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए मनुष्य को औषधि की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी यह कि मनुष्य अपने बुरे स्वभाव और मनोविकारों को ठीक कर ले।
साधारणतया समझाने-बुझाने की पद्धति ही सुधार परिवर्तन के लिए काम में लायी जाती है, पर देखा यह गया है कि भीतरी परतों पर जमे हुए कुसंस्कार इतने गहरे होते हैं कि उन पर समझाने-बुझाने का प्रभाव बहुत ही थोड़ा पड़ता है। नशेबाजी जैसी आदतों से ग्रसित व्यक्ति दूसरे अन्य समझदारों की तरह ही उस बुरी आदत की हानि स्वीकार करते हैं। दुःखी भी रहते हैं और छोड़ना भी चाहते हैं, पर उस आंतरिक साहस का अभाव भी रहता है जिसकी चोट से उस अभ्यस्त कुसंस्कारिता को निरस्तर किया जा सके। इस विवशता से कैसे छूटा जाय? इसका उपयुक्त उपाय सूझ ही नहीं पड़ता। लगता रहता है कि कोई दैवी दुर्भाग्य ऐसा पीछे पड़ा है जो विपत्ति से उबरने का कोई आधार ही खड़ा नहीं होने देता। पग-पग पर अवरोध ही खड़े करता और संकट पटकता भी वही दीखता है। यह दुर्भाग्य और कोई नहीं, अपने अंतरंग पर छाये हुए कषाय-कल्मष कुसंस्कार ही हैं, जो अभ्यास और स्वभाव का अंग बन जाने के कारण छुड़ाये नहीं छूटते और पटक-पटककर मारते हैं। नरक के यमदूतों जैसा त्रास देते हैं। इस विषमता को उलटने का समर्थ उपचार आंतरिक परिशोधन ही है। इस अंतस् कायाकल्प के लिए जितने भी उपाय खोजे गये हैं, उनमें तत्वदर्शियों ने अपने अनुभवों के आधार पर साधना तपश्चर्या को अत्यन्त प्रभावशाली पाया है। इनमें चान्द्रायण साधना को तो और भी अधिक महत्व दिया गया है। दुष्कृत्यों के निवारण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति अध्यात्म चिकित्सा ही है, यह तथ्य भली-भांति समझ लिया जाय।
कुकृत्यों को शासकीय एवं सामाजिक नियंत्रण के आधार पर बहुत कुछ काबू में रखा जा सकता है। मानसिक दुश्चिन्तन को दूरदर्शी विवेकशीलता के सहारे घटाया या हटाया जा सकता है, पर इतने से भी कुछ काम चलने वाला नहीं है क्योंकि प्रेरणाओं का उद्गम स्रोत तो अन्तःकरण में उठने वाली दुर्भावनाएं, आदर्शों के प्रति अनास्थाएं ही होती हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष में उसी की चित्र-विचित्र भूमिकाएं अनेकानेक कुकर्मों एवं दुर्घटनाओं के रूप में सामने आती रहती हैं। वास्तविक उपचार इसी क्षेत्र का होना चाहिए।
शरीर की रुग्णता, मन की उद्विग्नता, आर्थिक दरिद्रता, व्यक्तित्व का पिछड़ापन, पारिवारिक मनोमालिन्य, सम्पर्क क्षेत्र का विग्रह, साथियों की अवमानना जैसे संकटों के कारण तो सामयिक भी होते हैं और उनके लिए दोषी कइयों को ठहराया जा सकता है किन्तु वास्तविकता तलाशने पर प्रतीत होता है कि यह समस्त संकट एक ही थैली के चट्टे-बट्टे है, वे एक ही भानुमती के पिटारे से निकले हैं। विष वृक्ष की जड़ें कटनी ही चाहिए, टहनी मरोड़ने भर से कुछ काम चलने वाला नहीं है। न तो चिकित्सक के काबू में रोग आने वाले हैं और न उपदेशक, मनोवैज्ञानिक मानसिक विक्षोभों का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि वे जिस उद्गम स्रोत से निकलते हैं, वहां उभार उफनता ही रहा तो बाहरी रोकथाम से क्या बनेगा, एक छेद रोकते-रोकते दूसरा फूट पड़ेगा, मेंड़ बांधते और टूटते रहने का सिलसिला तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि उफान उत्पन्न करने वाला स्रोत बन्द नहीं हो जाता।
शरीर और मन के रोगों की रोकथाम के लिए कई प्रकार के उपचार, उपकरण एवं विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकते हैं किन्तु अन्तःस्थल की गहराई में पहुंचकर वहां कुछ उलट-पुलट करनी हो तो फिर अध्यात्म चिंतन एवं साधनात्मक उपचार ही एकमात्र अवलम्बन रह जाता है। ‘योग’ भावनाओं को उत्कृष्टता के साथ जोड़ता है और ‘तप’ कुसंस्कारिता को गलाकर सुसंस्कारिता में ढालने वाली भट्टी का प्रयोजन पूर्ण करता है।
इन आवश्यकताओं की पूर्ति जिन साधना उपचारों से हो सकती है उनमें कल्प साधना सर्वोपरि है। उसकी निर्धारित कार्य पद्धति का प्रभाव आरोग्य रक्षा, मनोयोग चिकित्सा के रूप में ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर अन्तराल की गहरी परतों में जमी हुई कुसंस्कारिता को उखाड़ फेंकने की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। एकांगी साधनाएं तो कितनी ही प्रचलित हैं, जिनमें परिशोधन और प्रगति परिष्कार के दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। जो एक होते हुए भी अनेक प्रयोजन सिद्ध कर सके ऐसी अध्यात्म चिकित्सा प्रस्तुत कल्प साधना के अतिरिक्त दूसरी कोई परिलक्षित नहीं होती।
Write Your Comments Here:
- अध्यात्म क्षेत्र की उच्चस्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग
- कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
- साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलम्बन
- आन्तरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता
- कर्मफल की सुनिश्चतता : एक महत्वपूर्ण तथ्य
- दुष्कृतों के अवरोधों को हटाने की साहसिकता उभरे
- पापों का प्रतिफल और प्रायश्चित-शास्त्र अभिमत
- समस्त व्याधियों का निराकरण— आध्यात्म उपचार से
- प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
- हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
- क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
- कल्पकाल की आहार साधना
- आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
- अन्तर्मुखी प्रवृत्ति और निरन्तर आत्म-दर्शन
- जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
- आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन
- कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं
- कल्पकाल की अति फलदायी ऐच्छिक साधनायें
- आहार एवं औषधिकल्प के मूल सिद्धांत एवं व्यावहारिक स्वरूप
- आहार सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियां एवं उनका निवारण
- कल्प के पूर्व कुछ अनिवार्य ज्ञातव्य
- कल्प चिकित्सा की पात्रता के सम्बन्ध में महर्षि चरक का मत
- विभिन्न प्रकार के कल्प प्रयोग
- कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार