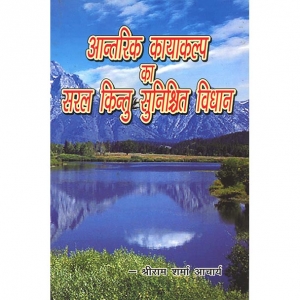आन्तरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिश्चित विधान 
क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
Read Scan Versionक्षतिपूर्ति को शास्त्रकारों ने इष्टापर्ति का नाम दिया है और उसे चान्द्रायण कल्प साधना के साथ एक अनिवार्य अंग के रूप में जोड़ा है।
क्षतिपूर्ति दो माध्यमों से होती है। (1) समयदान, श्रमदान, (2) साधनदान, अर्थदान। श्रमदान के रूप में धर्म प्रचार की पदयात्रा को तीर्थ-यात्रा कह कर उसकी आवश्यकता बताई गई है। तीर्थयात्रा मात्र देव प्रतिमाओं के दर्शन, नदी, सरोवरों के स्नान को नहीं कहते। उच्चस्तरीय उद्देश्य के निमित्त परिभ्रमण करना, जनसम्पर्क और सत्प्रवृत्तियों के बीजारोपण, अभिवर्धन के लिए प्रबल प्रयास करना ही तीर्थयात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। आज उसका स्वरूप जो भी बन गया हो, पर शास्त्र मर्यादा में तीर्थ यात्रा में पदयात्रा का ही उद्देश्य था। छोटे-छोटे विराम, विश्राम के रूप में ऐतिहासिक पुण्य स्थानों में कुछ समय ठहरना और वहां की पुरातन परम्परा का सान्निध्य प्राप्त करना उचित तो है, पर पर्याप्त नहीं। सच्ची तीर्थयात्रा लकीर पीटने, पर्यटन का मनोरंजन करने जैसी उथली नहीं हो सकती, उसके साथ कारगर परमार्थ प्रयत्नों को जुड़े हुए होना ही चाहिए।
श्रमदान में श्रेष्ठ कामों के लिए शारीरिक श्रम किया जाता है। मिलजुल कर कितने ही सामूहिक प्रयत्न सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन के लिए, रचनात्मक-सुधारात्मक प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाने के लिए किये जाने चाहिए। इन दिनों तो उनकी नितान्त आवश्यकता है। सामूहिक श्रमदान से रीछ-वानरों का पुल बांधना, ग्वाल-बालों का गोवर्धन उठाना प्रख्यात है। ऐसे-ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रज्ञा अभियान के अन्तर्गत जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ सामूहिक रूप से करने के लिए हैं अथवा हजारों किसान द्वारा किये गये वृक्षारोपण प्रयास की तरह एकाकी भी किए जा सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, प्रतिभापरक, प्रभाव क्षेत्र में प्रेरणादायक स्तर के अनेक प्रकार के श्रमदान हैं। अपने शरीर, मन, कौशल एवं प्रभाव के द्वारा स्वयं कुछ महत्वपूर्ण काम करना एवं दूसरों से करा लेना—यह सभी प्रयास श्रमदान की परिधि में आते हैं। इन प्रयोजनों के लिए कहीं भी जाना, किसी से भी सम्पर्क साधना तीर्थ यात्रा के पुण्य फल में सम्मिलित है।
क्षतिपूर्ति का दूसरा प्रकार है—साधन दान। उपार्जित सम्पदा का कोई महत्वपूर्ण अंग सत्प्रयोजनों में लगा देना अंशदान है। साधनदान को अंशदान कहा गया है, धनदान नहीं। अंशदान का अर्थ होता है—अपने संचय में से किसी अनुपात में त्याग किया जाना। पेट भरने लायक दो रुपया रोज कमाने वाले द्वारा एक समय भूखा रहकर एक रुपया बचाना और उसे परमार्थ में लगा देना आधा अंशदान हुआ। दस लाख की पूंजी वाले का दस रुपया लगाना अनुपात की दृष्टि से एक लाखवां भाग हुआ। इस दृष्टि से अंशदान हजार गुना अधिक पुण्यफल दायक है।
अध्यात्म क्षेत्र में साधनदान में धनराशि के विस्तार की कोई गणना महत्ता नहीं। परखा यह जाता है कि परिस्थितियों की तुलना में किसकी उदारता का स्तर कितना बढ़ा-चढ़ा है। किसने कितनी कृपणता त्यागी और कितनी उदार परमार्थ परायणता अपनाने में किस अनुपात में त्याग करने का साहस दिखाया।
परमार्थ प्रयोजनों में कभी अन्नदान, वस्त्रदान, औषधिदान, निर्धनों एवं कष्ट पीड़ितों की सुविधा के लिए किया जाता था। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता था कि पीड़ा और पतन का एकमात्र कारण मनुष्य का पिछड़ा-पतनोन्मुख व्यक्तित्व ही है। उसे ऊंचा उठाने में संलग्न सद्ज्ञान की प्रेरणा एवं सत्कर्म की धर्मधारणा का महत्व जड़ सींचने के समान है। तात्कालिक एवं सांसारिक कष्ट दूर करने के लिए अस्पताल और सुख-सुविधा सम्वर्धन के लिए उद्यान, तालाब बनाने जैसे कार्य मात्र शरीर क्षेत्र की पदार्थ परक सुख-सुविधाएं ही बढ़ाते हैं। चींटी को आटा, गाय को चारा, कौए को पिण्ड खिलाना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतोष उपार्जन करने का एक हल्का-फुल्का तरीका है। अन्यथा उपयोगिता की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं। वे प्राणी अपने पुरुषार्थ से अपना गुजारा बड़े मजे में कर लेते हैं। बिना आवश्यकता वाले पर दान थोपना ऐसा ही है जैसा कि करोड़पति मठाधीशों अथवा स्वर्ण जटित देवालयों पर दान-दक्षिणा का भार लादकर उन्हें किसी और अपव्यय के लिए उत्तेजित करना।
आज की स्थिति में सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकने वाला समस्त समस्याओं का समाधान करने वाला एक ही प्रयोजन है—प्रज्ञा विस्तार, सद्भाव सम्वर्धन की पृष्ठभूमि बनाना और अज्ञानान्धकार को मिटाने के लिए युग चेतना के दीपक जलाना। प्रज्ञा अभियान के अन्तर्गत ऐसे अनेक प्रयोजन हैं जिन्हें निश्चित रूप से ब्रह्मदान कहा जा सकता है। ब्रह्मदान को अन्य समस्त दानों की तुलना में सहस्र गुना अधिक पुण्य फलदायक बताया गया है। इन दिनों किसी प्रायश्चित कर्त्ता को अंशदान करना हो तो उसे जनमानस के परिष्कार, सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन, आलोक वितरण को ही प्रमुखता देनी चाहिए।
देव दक्षिणा जिसे पूर्णाहुति इष्टापूर्ति का अंग माना जाता है, को इस प्रकार साधक सम्पादित करते रह सकते हैं—
आत्म–निर्माण के दो चरण—
(1) साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का दिनचर्या में समावेश और निर्वाह।
(2) परिवार में सुसंस्कारिता के प्रचलन। श्रमशीलता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, सज्जनता एवं उदार सहकारिता का परिजनों को अभ्यास कराना।
लोक निर्माण के दो प्रयास—
(1) अंशदान अर्थात् आजीविका का एक अंश प्रज्ञा प्रसार के लिए नियमित रूप से निकालना। न्यूनतम दस पैसा नित्य और महीने में एक दिन की कमाई।
(2) समयदान अर्थात् न्यूनतम एक घण्टा नित्य और सामान्यतया इसके अतिरिक्त अवकाश के दिन भी प्रज्ञा अभियान को अपने क्षेत्र में विस्तृत करना तथा रचनात्मक सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए नियोजित करना।
साधना में नियमित गायत्री उपासना न्यूनतम एक माला का जप तथा प्रातःकालीन सूर्य की प्रकाश किरणों के आत्मसत्ता में अवतरण का ध्यान, गुरुवार या रविवार को आधे दिन का उपवास अथवा अस्वाद व्रत। महीने में एक दिन चौबीस आहुतियों का हवन।
स्वाध्याय में नित्य-नियमित रूप से प्रज्ञा साहित्य न्यूनतम आधा घण्टा पढ़ना। युग सृजन के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए यथा सम्भव प्रयत्न।
परिवार निर्माण के लिए स्वयं आगे रहकर अन्य परिजनों को साथ लेना और पंचशीलों को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर योजनाबद्ध प्रयास करते रहना है।
इस प्रकार इस जन्म के विस्मृत एवं पूर्व जन्म के संचित पापों से निवृत्ति का श्रेष्ठतम मार्ग देव दक्षिणा ही हो सकता है।
पापों के विषय में भी जनमानस की अनेकानेक भ्रान्तियां हैं। मात्र प्रत्यक्ष ही नहीं, दृष्टिगोचर न होने वाले परोक्ष दुष्कृत्य भी पाप माने जाते हैं। पाप शारीरिक भी होते हैं, मानसिक और आर्थिक भी। लोग चोरी, डकैती जैसे शरीरजन्य पापों को ही पाप मानते हैं क्योंकि कानून में जिन्हें अपराध माना गया है लोक प्रचलन में भी उनकी भर्त्सना होती है। आर्थिक पापों में न केवल ठगी, मिलावट आदि की गणना है वरन् अनुचित माध्यमों से कमाना और उसका अनावश्यक संग्रह एवं अवांछनीय अपव्यय करना भी आर्थिक पापों में गिना जाता है। मानसिक पापों में अनुपयुक्त चिंतन ही नहीं वरन् दूसरों को अनैतिक परामर्श देना, अनुचित कामों का समर्थन-सहयोग करना भी इसी श्रेणी में आता है। राग-द्वेष की, लोभ-मोह की, वासना-तृष्णा की अमर्यादित स्थिति भी अध्यात्म निर्धारण के अनुसार पाप कर्मों में ही सम्मिलित होती है। इन सभी के दुष्परिणाम होते हैं। अस्तु प्रायश्चित की बात सोचते समय, क्षति पहुंचाने का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते समय न केवल बहुचर्चित अपराधों पर विचार करना चाहिए वरन् यह भी देखना चाहिए कि मानसिक, आर्थिक अपराध कितने और किस स्तर के बन पड़े। यों जीवन सम्पदा ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिए दी थी उसे भुलाकर उस अमानत को निकृष्ट प्रयोजनों से विभिन्न कामों में खर्च करना भी ‘अमात में खयानत’ जैसा पाप है। शास्त्रकारों ने इसे आत्महत्या एवं ब्रह्महत्या का नाम दिया है। आत्म कल्याण का मार्ग अवरुद्ध रखे रहना स्पष्टतः जीवन देवता का, भगवान का तिरस्कार, अपमान है। इसे भी हल्का पाप नहीं मानना चाहिए।
पाप कर्मों का प्रायश्चित एवं पश्चात्ताप वर्ग की पूर्ति व्रत उपवास से, शारीरिक कष्ट सहने से, तितिक्षा कृत्यों से होती है। किन्तु क्षति पूर्ति का प्रश्न फिर भी सामने रहता है। इसके लिए पुण्य कर्म करने होते हैं, ताकि पाप के रूप में जो खाई खोदी गई थी वह पट सके, पुण्य-पाप का पलड़ा बराबर हो सके। दुष्प्रवृत्तियों को सत्प्रवृत्तियों से ही पाटा जा सकता है। इसलिए दुष्कर्म करके जो व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाई गई, समाज में भ्रष्ट अनुकरण की परम्परा चलाई गई, वातावरण में विषाक्त प्रवाह फैलाया गया उसको निरस्त तभी किया जा सकता है, जब सत्प्रयोजनों को संवर्धित करने वाले पुण्य कर्म करके उसकी पूर्ति की जाय, समाज को सुखी और समुन्नत बनाने वाली सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन आवश्यक माना जाय। इसके लिए समय, श्रम एवं मनोयोग लगाया जाय।
व्यभिचारजन्य पापों का प्रायश्चित यही है कि नारी को हेय स्थिति से उबारने के लिए उसे समर्थ और सुयोग्य बनाने के लिए जितना पुरुषार्थ बन पड़े उसे लगाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न किया जाय।
आर्थिक अपराधों का प्रायश्चित यह है कि अनीति उपार्जित धन उसके मालिक को लौटा दिया जाय अथवा सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन के श्रेष्ठ कामों में उसे लगा दिया जाय।
घटनाओं की क्षति पूर्ति अर्थ दण्ड सहने से भी हो सकती है। रेल दुर्घटना आदि होने पर मरने वालों के घर वालों को सरकार अनुदान देती है। उसमें क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक प्रावधान को भी एक उपाय माना गया है। प्रायश्चित विधानों में क्षतिपूर्ति की दृष्टि से दान को महत्व दिया गया है। शास्त्र कहता है।
सर्वस्वदानं विधिः सर्वपापविशोधनम् ।
—कूर्म पुराण
अनीति से संग्रह किए हुए धन को दान कर देने पर ही पाप का निवारण होता है।
दत्वैवापहृतं द्रव्यं धनिकस्याभ्युपापतः ।
प्रायश्चित्तं ततः कुर्यात कलुषस्य पापनुत्तपे ।।
—विष्णु स्मृति
जिसका जो पैसा चुराया हो, उसे वापिस करे और उस चोर कर्म का प्रायश्चित करे।
वापिसी सम्भव न हो या आवश्यक न हो तो अनीति उपार्जित साधनों का बड़े से बड़ा अंश श्रेष्ठ सत्कर्मों में लगा देना चाहिए।
आचार्य वृहस्पति के अनुसार—
उपवासस्तथादानं उभौ अन्योन्याश्रितः ।
अर्थात्—प्रायश्चित में उपवास की तरह दान भी आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं।
प्राज्ञ-प्रतिग्रहं कृत्वा तद्धनं सद्गतिं नयेत् यज्ञाद्वा पतितोद्धार पुण्यात् न्यायरक्षणेवापीकूप तड़ागेषु ब्रह्मकर्म समत्सृजेत् ।
—अरुण स्मृति
अनुचित धन जमा हो तो उसे यज्ञ, पतितोद्धार, पुण्य कर्म, न्याय रक्षार्थ, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण एवं ब्रह्म कर्मों में लगा दें। अनुचित धन की सद्गति इस प्रकार होती है।
तेनोदपानं कर्त्तव्यं रोपणीयस्तथावटः ।
—शाततप
तालाब खुदवा कर बरगद का पेड़ लगा देना चाहिए।
सच्छास्त्रपुस्तकम् दद्यात् विप्राय सदक्षिणाम् ।
—पाराशर
ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित श्रेष्ठ ग्रन्थ देना चाहिए।
वापीकूपतड़ागादि देवतायतनानि च ।
पतितान्युद्धरेयस्तु व्रतपूर्ण समाचरेत् ।।
—यम.
बावड़ी, कुआं, तालाब, देवमंदिर और जीर्णाद्धार आदि कार्य को व्रतपूर्ण स्थिति में करे।
सोऽपि पापविशुद्धार्थ चरेच्चान्द्रायणं व्रतम् ।
व्रतान्ते पुस्तकं दद्यात् धेनुं वत्ससमन्वितम् ।।
—शात्तायन.
पापों की शुद्धि के लिए चान्द्रायण व्रत करे और व्रत के अन्त में श्रेष्ठ ग्रन्थ और बछड़े सहित गौ दान करे।
सुवर्ण गोदानं भूमिदानं तथैव च ।
नाशयन्त्याशु पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि ।।
—सम्वर्त.
सुवर्ण का दान, गौदान एवं भूमिदान शीघ्र ही पूर्व जनम के पापों को नष्ट कर देते हैं।
इन अभिवचनों में सत्साहित्य वितरण, विद्यादान, वृक्षारोपण, कुआं, तालाब, देवालय आदि का निर्माण-यज्ञ, दुःखियों की सेवा, अन्याय पीड़ितों के लिए संघर्ष आदि अनेक शुभ कर्मों में क्षति की पूर्ति के रूप में अधिक से अधिक उदारतापूर्वक दान देने का विधान है। इस दान शृंखला में गौदान को विशेष महत्व दिया गया है।
पाप निवृत्ति और पुण्य वृद्धि के दोनों प्रयोजनों की पूर्ति के लिए तीर्थयात्रा को शास्त्रकारों ने प्रायश्चित तप साधना में सम्मिलित किया है। तीर्थयात्रा का मूल उद्देश्य है धर्म प्रचार के लिए पदयात्रा। दूर-दूर क्षेत्रों में जन सम्पर्क साधने और धर्म धारणा को लोक-मानस में हृदयंगम कराने का श्रमदान तीर्थयात्रा कहलाता है। श्रेष्ठ सत्पुरुषों के सान्निध्य में प्रेरणाप्रद वातावरण में रहकर आत्मोत्कर्ष का अभ्यास करना भी तीर्थ कहलाता है। यों गुण, कर्म, स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए किये गये प्रबल प्रयासों को भी तीर्थ कहते हैं। प्रायश्चित विधान में इसी प्रकार की सार्थक तीर्थयात्रा की आवश्यकता बताई गई है।
आज की तथाकथित तीर्थयात्रा मात्र देवालयों के दर्शन और नदी सरोवरों के स्नान आदि तक सीमित रहती है। यह पर्यटन मात्र है। इतने भर से तीर्थयात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। सत्प्रवृत्तियों के सम्वर्धन के लिए किया पैदल परिभ्रमण ही तीर्थयात्रा कहलाता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्वर्धन के लिए श्रेष्ठ उपचार भी है। धर्म प्रचार के लिए जन-सम्पर्क साधने का पैदल परिभ्रमण जन समाज को उपयुक्त प्रेरणायें प्रदान करता है। साथ ही उससे श्रमदान कर्त्ता की सत्प्रवृत्तियों का सम्वर्धन भी होता चलता है। ऐसे ही अनेक कारणों को ध्यान में रखकर तीर्थयात्रा को ऐसा परमार्थ कहा गया है जिसे कर सकना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव हो सकता है। तीर्थयात्रा का स्वरूप और महात्म्य शास्त्रकारों ने इस प्रकार बताया है—
नृणां पापकृतां तीर्थो पापस्य शमनं भवेत् ।
यथोक्त फलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् ।।
पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल देने वाला है।
तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्धायुक्तं समाहितः ।
कृतपापों विशुद्धश्चे किं पुनः शुद्ध कर्मकृत ।।
जो तीर्थों का सेवन करने वाला धैर्यवान्, श्रद्धायुक्त और एकाग्र चित्त है वह पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है, फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है, उसकी तो बात ही क्या है।
तीर्थानि च यथोक्तेन विधिनां संचरन्ति ये ।
सर्वद्वन्द्वसहा धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ।।
जो यथोक्त विधि से तीर्थयात्रा करते हैं, सम्पूर्ण द्वन्द्वों को सहन करने वाले हैं, वे धीरे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं।
यावत् स्वस्थोऽस्ति मे देहो यावन्नेन्द्रियविक्लवः ।
तावत् स्वश्रेयसां हेतु तीर्थयात्रां करोम्यहम् ।।
जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, जब तक आंख, कान आदि इन्द्रियां सक्रिय हैं, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए तीर्थयात्रा करते रहने का निश्चय करता हूं।
क्रिया कर्मेण महता तपसा नियमेन च ।
दानेन तीर्थयात्राभिश्चिरकालं विवेकतः ।।
दुष्टकृतैः क्षयमाप्न्ने परमार्थ विचारणे ।
काकतालीय योगेन बुद्धिर्जन्तो प्रवर्तते ।।
बहुत दिनों तक यज्ञ-दानादि करने से, कठिन तपस्या, नियमपालन, तीर्थयात्रा आदि से विवेक बढ़ता है और इनके द्वारा बुरे कर्मों का नाश हो जाने पर, काकतालीय न्याय से मनुष्य में परमार्थ बुद्धि प्रस्फुटित हो जाती है।
इतना भर हो सके तो यह सोचा जा सकता है कि प्रगति की दिशा में कुछ कदम चल पड़े। सतत् अभ्यास से चिंतन एवं कृत्य भी उसी रंग में रंगने लगते हैं। अपना आपा विस्तृत नजर आता है और उदार आत्मीयता का विस्तार होने लगता है।
प्रायश्चित के रूप में कल्प साधना की की पूर्णाहुति में इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए जो सम्भव हो, वह करना चाहिए। मात्र भोजन में थोड़ी कटौती करने और कुछ घण्टों की पूजा-उपासना को ही कल्प तपश्चर्या की इतिश्री नहीं मान लेना चाहिए।
Write Your Comments Here:
- अध्यात्म क्षेत्र की उच्चस्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग
- कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
- साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलम्बन
- आन्तरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता
- कर्मफल की सुनिश्चतता : एक महत्वपूर्ण तथ्य
- दुष्कृतों के अवरोधों को हटाने की साहसिकता उभरे
- पापों का प्रतिफल और प्रायश्चित-शास्त्र अभिमत
- समस्त व्याधियों का निराकरण— आध्यात्म उपचार से
- प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
- हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
- क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
- कल्पकाल की आहार साधना
- आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
- अन्तर्मुखी प्रवृत्ति और निरन्तर आत्म-दर्शन
- जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
- आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन
- कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं
- कल्पकाल की अति फलदायी ऐच्छिक साधनायें
- आहार एवं औषधिकल्प के मूल सिद्धांत एवं व्यावहारिक स्वरूप
- आहार सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियां एवं उनका निवारण
- कल्प के पूर्व कुछ अनिवार्य ज्ञातव्य
- कल्प चिकित्सा की पात्रता के सम्बन्ध में महर्षि चरक का मत
- विभिन्न प्रकार के कल्प प्रयोग
- कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार