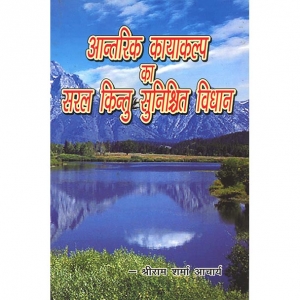आन्तरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिश्चित विधान 
कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
Read Scan Versionयह एक सुविदित तथ्य है कि संचित पापकर्मों का प्रतिफल रोग, शोक, विक्षोभ, हानि एवं विपत्ति आदि के रूप में उपस्थित होता है। विपत्तियों को भुगतने का मूल आधार मनुष्य का भ्रष्ट चिन्तन एवं दुष्ट आचरण ही होता है। पापकर्म के बीज सर्वप्रथम दुष्प्रवृत्ति बनकर अंकुर की तरह उगते हैं। उसके बाद वे पेड़-पौधे बनकर फलने-फूलने योग्य जब तक नहीं होते तब तक उनका स्वरूप पतन-पराभव के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले दुराचरण जैसा होता है। कालान्तर में जब वे परिपुष्ट, परिपक्व हो जाते हैं तो आधि-व्याधि, विपत्ति, हानि, भर्त्सना के रूप में कष्ट देने लगते हैं। दुष्कर्मों के अवश्यंभावी प्रतिफल से बचने का दैवी प्रकोप एवं सामाजिक प्रताड़ना के अतिरिक्त दूसरा मार्ग प्रायश्चित का है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य आत्मशोधन और आत्म परिष्कार का दुहरा प्रयोजन एक साथ पूरा कर सकता है।
प्रगति पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को जो तप साधना करनी पड़ती है उसके स्वरूप दो ही हैं। पहला है—आंतरिक अवरोधों से पीछा छुड़ाया जाय और दूसरा है—आत्मबल पर आश्रित अनुकूलताओं को अर्जित किया जाय। यही है आत्मिक पुरुषार्थ का एक मात्र और वास्तविक स्वरूप। यात्री को एक पैर उठाना और दूसरा बढ़ाना पड़ता है। उठाने का तात्पर्य है—कुसंस्कारों को छोड़ा जाय, उसके लिए कठोर तप किया जाय। बढ़ाने का अर्थ है—सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव एवं आचरण में घुला दिया जाय। कच्ची धातुयें अपनी सामान्य स्थिति में प्रयुक्त नहीं होतीं। उन्हें बहुमूल्य उपकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रचण्ड ताप की भट्टी द्वारा गलाई-ढलाई करनी पड़ती है। गलाई को ‘तप’ और ढलाई को ‘योग’ कहते हैं।
उपवास एवं सुसंस्कारी अन्न से काय शोधन होता है और मनःक्षेत्र में प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। शरीर कल्प के यही दो आधार हैं। आत्मिक कायाकल्प के लिए भी शरीर का तप तितिक्षा के आधार पर ही परिशोधन होता है। यह प्राथमिक अनिवार्यता मानी जानी चाहिए। उपवास पर आधारित आहार चिकित्सा को कायिक निरोगता का मूल आधार माना जा सकता है। पेट का भार हल्का रहने और सहकारी न्यूनतम आहार से गुण, कर्म, स्वभाव पर उपयोगी प्रभाव पड़ने का प्रत्यक्ष लाभ स्वास्थ्य सुधार के रूप में दृष्टिगोचर होता है।इसी प्रकार इन्द्रिय संयम, अर्थ-संयम और विचार संयम का अभ्यास करने से अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। अन्धकार हटना और प्रकाश बढ़ना एक ही बात है। कुसंस्कार घटेंगे तो आंतरिक प्रखरता स्वयमेव बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त उन दिनों आंतरिक परिवर्तन हेतु जो भावनात्मक प्रयत्न होते हैं और योगाभ्यास सम्मत अतिरिक्त प्रयास भी चलते हैं, वह अभ्युदय-उत्कर्ष की सशक्त प्रक्रिया है।
अन्न को वस्तुतः ब्रह्म एवं प्राण की उपमा दी गयी है। उपनिषद्कार ने अन्न ब्रह्म की उपासना करने के लिए साधकों को सहमत करने पर अनेकानेक तर्क, तथ्य एवं प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। आमतौर से आहार द्वारा क्षुधानिवृत्ति एवं स्वाद तृप्ति भर की बात सोची जाती है। वास्तव में यह मान्यता सर्वथा अधूरी है। भोजन प्रकारान्तर से जीवन है। उसकी आराधना ठीक प्रकार की जा सके तो शरीर को आरोग्य, मस्तिष्क को ज्ञान-विज्ञान, अन्तःकरण को देवत्व के अनुदान, व्यक्तित्व को प्रतिभा तथा भविष्य को उज्ज्वल सम्भावनाओं से जाज्वल्यमान बनाया जा सकता है।
मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है ‘‘जैसा खाये अन्न वैसा बने मन’’। यहां अन्न से अर्थ है साधक का आहार। आहार शुद्धि साधना का प्रथम चरण है। तमोगुणी, उत्तेजक, अनीति उपार्जित, कुसंस्कारियों द्वारा पकाया-परोसा भोजन न केवल मनोविकार ही उत्पन्न करता है वरन् रक्त को अशुद्ध व पाचन को विकृत करके स्वास्थ्य संकट भी उत्पन्न करता है। आत्मिक प्रगति में, साधना की सफलता में तो कुधान्य का, अभक्ष्य का प्रभाव विषवत् पड़ता है। मन की चंचलता इतनी अधिक हो जाती है कि सामान्य कार्यों में भी एकाग्र हो पाना सम्भव नहीं हो पाता। फिर साधना में अभीष्ट मनोयोग तो आहर शुद्धि बिना कैसे प्राप्त हो?
पिप्लाद ऋषि पीपल वृक्ष के फल खाकर निर्वाह करते थे। कणाद ऋषि जंगली धान्य समेटकर उससे क्षुधा शांत करते थे। भीष्म पितामह शर शैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश दे रहे थे, तब द्रौपदी ने पूछा—‘‘देव, जब मुझे भरी सभा में नग्न किया जा रहा था तब आपने कौरवों को यह उपदेश क्यों नहीं दिये?’’ वे बोले—‘‘उन दिनों मेरे शरीर में कुधान्य से उत्पन्न रक्त बह रहा था, अस्तु बुद्धि भी वैसी ही थी। अब घावों के रास्ते वह रक्त निकल गया और मेरी स्थिति सही सोचने एवं सही परामर्श देने जैसी बन गई है।’’ रुक्मिणी का जंगली बेर खाकर तथा पार्वती का सूखे पत्तों पर रहकर तप करना प्रसिद्ध है। उच्चस्तरीय साधनाओं में व्रत उपवास का अविच्छिन्न स्थान है। साधना में मन का सात्विक होना आवश्यक है। मन को शान्त, स्थिर एवं सात्विक बनाने के लिए उपवास पर, अन्न की सात्विकता पर ध्यान देना अति आवश्यक है।
कल्प साधना वस्तुतः उपवास प्रधान है। इसका एक स्वरूप चान्द्रायण साधना के रूप में देखने को मिलता है। चान्द्रायण का सर्वविदित नियम-अनुशासन पूर्णिमा से अमावस्या तक भोजन घटाने और तदुपरांत क्रमशः बढ़ाते हुए अगली पूर्णिमा को नियत मात्रा तक ले पहुंचना है। इसमें मन का कठोर संयम जिस प्रकार सम्भव हो पाता है, वह अन्य साधनाओं में नहीं है। यह क्रम पुरातन काल के साधकों के मनोबल और उनकी शरीरगत सामर्थ्य को देखकर ठीक भी था, पर अब बदली परिस्थितियों में जहां मनुष्य की जीवनी शक्ति उतनी नहीं रही, पर्यावरण के परिवर्तन उसे जल्दी-जल्दी प्रभावित भी करते हैं, उतनी कठोर साधना सम्भव नहीं। फिर भी उपवास का महत्व जहां का तहां रहेगा। आरोग्य रक्षा की दृष्टि से भी अन्य श्रमिक-मजदूरों की तरह पेट को सप्ताह में एक बार छुट्टी मिलनी ही चाहिए। ऐसा न रहने पर उसकी कार्य क्षमता घटती है तथा शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्र होते चले जाते हैं। पूर्ण उपवास न बन पड़े तो कम से कम यह सम्भव है कि कल्प की अवधि में आधे या कम आहार पर निर्वाह कर लिया जाय। शाकाहार, फलाहार, अन्नाहार में से किसी एक को चयन कर उसे ही नियत मात्रा में नित्य लेते रहने का भी चान्द्रायण साधना में प्रावधान है। इसे एक प्रकार का मृदु चान्द्रायण कहा जा सकता है। भांति-भांति के सम्मिश्रणों से बचकर साधक यदि एक ही अन्न या शाक पर कल्प कर ले तो आहार शुद्धि, आन्तरिक कायाकल्प, आरोग्य प्राप्ति के सभी प्रयोजन पूरे होते हैं।
आहार इन दिनों जो लिया जाय, वह सामान्य से आधा या और भी कम हो। सात्विक हो, सुपाच्य हो। इसके लिए भाप के माध्यम से पकाये गये अन्न को वैज्ञानिक, शास्त्रीय दोनों ही मतों से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चिकनाई-मसाले और शक्कर, नमक आदि का आदि मन तथा शरीर उस ढर्रे को सहज ही तोड़ नहीं पाता। पर धीरे-धीरे कल्पकाल के शोधित-स्वादहीन आहार में ही ऐसी रुचि विकसित होने लगती है, मानो साधक प्रत्यक्ष औषधि ही अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रहण कर रहे हैं। सन्तुलित आहार के नाम पर विविधताएं जुटाना व्यर्थ हैं। हर उपयुक्त खाद्य पदार्थ में वे सभी तत्व पाये जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता है। निर्धारित कल्प साधना में ही हविष्यान्न, अमृताशन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि ऋषिधान्यों को अकेले अथवा शाकपत्तियों के साथ भाप के माध्यम से उबाल द्वारा पकाकर दिन में दो बार नियत से आधी मात्रा ग्रहण करने का प्रावधान है। इससे कम में वह मनोबल नहीं जुट पाता जो निष्कासन प्रक्रिया तथा नवीन निर्धारण-जीवन दृष्टि के विकास हेतु जरूरी है। आज की परिस्थितियों के अनुरूप यह साधना हर दृष्टि से साधक को आमूलचूल बदल देने वाली प्रक्रिया के लिए उसे समर्थ, शक्ति सम्पन्न बना देने वाली मानी जानी चाहिए।
आहार साधना के अतिरिक्त तप-तितिक्षा में प्रायश्चित की चर्चा की जाती है। अपना अन्तःकरण धोये बिना, विगत को भुलाये बिना साधन मात्र बाह्योपचार भर रह जाती है। ‘कल्प साधना’ का अर्थ ही यह है कि अन्दर से बाहर तक साधक पूरी तरह बदल जाये। पुरानी केंचुली निकाल फेंके, नूतन चोला पहने। प्रायश्चित इसीलिए किया जाता है और उसकी महत्ता को शास्त्रों ने इसी कारण अत्यधिक माना है, उस पर पूरा जोर दिया है।
प्रायश्चित में तीन पश्च हैं— एक- व्रत उपवास जैसी तितिक्षा, दूसरा- संचित कुसंस्कारों को उखाड़ने और उस स्थान पर उच्चस्तरीय शालीनता को स्थापित करने का अन्तर्मुखी पुरुषार्थ, तीसरा- खोदी हुई खाईं को पाटने वाली क्षति पूर्ति के लिए पुण्य पुरुषार्थ का उदार साहस। इन तीनों के संयुक्त समावेश से ही प्रायश्चित की पूर्ण प्रक्रिया सधती है। मात्र आहार करने भर से तो कल्प प्रक्रिया का एक छोटा भाग ही सधता है।
इस साधना को एक प्रकार के आयुर्वेदीय कायाकल्प उपचार के समान समूचे व्यक्तित्व का संशोधन-सम्वर्धन करने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। इतने पर भी कल्प के भौतिक सिद्धांत दोनों में ही एक जैसे हैं। एकांत सेवन, आहार संयम तथा निर्धारित चिन्तन यही आधान कल्प साधना के भी हैं। रोगी अपने रोग का स्वरूप ही नहीं, इतिहास भी चिकित्सक को बताता है। उसी निदान के आधार पर उपचार की व्यवस्था बनती है। कल्प प्रक्रिया में मार्गदर्शक को अपने संचित पाप कर्मों का विस्तृत वर्णन, स्वभावगत दोष-दुर्गुणों का परिचय एवं भौतिक, आत्मिक अवरोधों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। इन दोनों पक्षों पर गम्भीर विचार करने के उपरांत ही हर व्यक्ति को कुछ विशेष परामर्श दिये जाते हैं, उपाय-विचार बताये जाते हैं। कल्प साधना में सामान्य उपचार तो एक जैसे हैं किन्तु साथ ही हर साधक की स्थिति के अनुरूप उसे कुछ अतिरिक्त उपाय साधन भी बताये जाते हैं। इन निर्धारणों को कौतुक-कौतूहल एवं बेगार जैसी चिह्न पूजा नहीं बनाया जाता, लकीर पीटने भर की आधी-अधूरी, लंगड़ी-लूली प्रक्रिया अपनाने से इतना बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं होता। उसमें गम्भीर होना पड़ता है और निर्धारित अनुशासन का कठोरतापूर्वक परिपालन करना पड़ता है।
यह कल्प साधना घर के व्यस्त-अभ्यस्त वातावरण में नहीं हो सकती। उपवासपूर्वक अनुष्ठान तो आये दिन होते रहते हैं। अन्तः के कायाकल्प की साधना उससे आगे की चीज है, उसके लिए तद्नुरूप तीर्थ जैसा पवित्र वातावरण, उपयुक्त साधन एवं ऋषि कल्प मार्गदर्शन चाहिए। यह आवश्यकता शांतिकुंज गायत्री नगर में अच्छी तरह सम्पन्न हो सकती है वैसी सुविधा कहीं अन्यत्र मिल सकना कठिन है। पूर्ण कल्प साधना एक महीने की होती है और लघु ‘शिशु’ साधना दस दिन की। दोनों में समय का ही अन्तर है। विधान, अनुशासन दोनों में एक जैसे हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि शरीरगत अनुबन्धों की निर्धारित दिनचर्या अपनाये रहने के अतिरिक्त मानसिक स्थिति भी बनानी पड़ती है, मानो किसी अन्य लोक में उन दिनों रहा जा रहा है। इन दिनों सांसारिक चिन्तन एक प्रकार से विस्मृत ही कर देना चाहिए और मात्र अध्यात्म लोक की आवश्यकताओं तथा अन्तःक्षेत्र की समस्याओं का हल करने में ही चित्त को पूरी तरह केन्द्रित रखना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं इतनी विकट होती हैं कि उन्हें सुलझाने वाले साधन जुटाने में प्रायः समूची जीवन अवधि खप जाती है। फिर आत्मिक जीवन तो और भी व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। उसकी गुत्थियां सुलझाने और प्रगति के सरंजाम जुटाने हेतु नये सिरे से नये दृष्टिकोण तथा नया साहस जुटाना होता है। इतने बड़े काम के लिए निर्धारित साधना का स्वरूप यही है कि उसमें से भौतिक चिन्तन एवं प्रयोजनों में भी प्रयास के लिए तनिक भी कोशिश नहीं की जाय तथा मनोयोग को निर्धारित प्रयोजनों में जुटाये रखा जाय। मन को अन्य किसी कार्य में अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार चान्द्रायण साधना को ‘व्रत’, ‘तप’ एवं ‘कल्प’ के नाम से भी जाना जाता है। ‘व्रत’ अर्थात् संयम, अनुशासन, निर्धारण एवं परिपालन। ‘तप’ अर्थात् संचित कुसंस्कारों से संघर्ष और शालीनता के अवधारण का अभ्यास-पुरुषार्थ। ‘कल्प’ अर्थात् पिछली हेय स्थिति को उलट कर उस स्थान पर उत्कृष्टता का प्रतिष्ठापन। यह तीनों ही प्रयास परस्पर मिलते हैं तो ज्ञान और कर्म की गंगा-यमुना मिलने से एक नई धारा भक्ति भावना की, दिव्य जीवन की सरस्वती के रूप में उद्भूत होती है। इस समन्वय से त्रिवेणी संगम बनता है। उसका अवगाहन करने वाले इस धरती पर स्वर्ग का आनन्द लेते हैं, जीवनमुक्त बनते हैं और मनुष्य रूप में देवता कहलाते हैं। इसी परम लक्ष्य की पूर्ति करना आन्तरिक काया कल्प साधना का आधारभूत उद्देश्य है।
संक्षेप में कल्प साधना के तीन पक्ष हैं—संयम-साधना, प्रज्ञा-उपासना, भविष्य निर्धारण की आराधना। संयम साधना में उपवास प्रमुख है। इस अवधि में आहार सामान्य की तुलना में आधा ही लिया जाता है। जो खाया जाए वह पूर्ण सात्विक एवं सुसंस्कारी हो, इसका ध्यान रखा जाता है। संयम को ही तप कहते हैं। सामान्य जीवन में यह तप चार प्रकार का अपनाया जाता है। (1) इन्द्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य, मौन, अस्वाद आदि की तितिक्षा, (2) अर्थ संयम के लिए मितव्ययिता। परिश्रमशीलता अपनाकर सादा जीवन उच्च विचार का अभ्यास, औसत भारतीय स्तर के निर्वाह का अभ्यास, (3) समय संयम-एक घड़ी भी आलस्य प्रमाद में बर्बाद न होने देना। दिनचर्या बनाकर उसके परिपालन में तत्परता बरतना, (4) विचार चिन्तन को अस्त-व्यस्त उड़ाने भरने से रोकना, सौंपे हुए काम में ही मनोयोग नियोजित रखना। चान्द्रायण में यह चारों ही संयम साधनाएं तपश्चर्या के रूप में निर्धारित करनी होती हैं। तपस्वी सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान् बनता है। उसकी ऊर्जा से प्रखरता, परिपक्वता बढ़ती है। तपस्वी ही शरीरगत ओजस्, तेजस् एवं अन्तःकरण के वर्चस् से सुसम्पन्न बनते हैं। इसी आत्मबल के सहारे ऋद्धि-सिद्धियों का द्वार खुलता है। प्रज्ञा उपवास में गायत्री पुरश्चरण मुख्य है। ढाई घण्टा नित्य का समय इसके लिए नियत है। इसी बीच निर्धारित जप संख्या पूरी की जाए। साथ ही प्रभात कालीन सूर्य किरणों के तीनों शरीर में प्रवेश करने का ध्यान किया जाए। अनुभव किया जाए कि गायत्री के प्राण सविता देवता का दिव्य आलोक जीवन सत्ता के कण-कण में प्रवेश करके तीन अनुदान प्रदान करता है—स्थूल शरीर में सद्कर्म, सूक्ष्म शरीर में सद्ज्ञान, कारण शरीर में सद्भाव। इन्हीं तीनों को क्रमशः निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा भी कहते हैं। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग के अन्तर्गत इन्हीं दिव्य अनुदानों का विवेचन किया जाता है और तृप्ति, तुष्टि, शांति की त्रिविध विभूतियों के सहारे देवोपम जीवन जी सकने का लाभ समझाया जाता है। जिनको यह दिव्य सम्पदा जितनी मात्रा में उपलब्ध होती है, वह उसी अनुपात में आत्म सन्तोष, जन सहयोग एवं दैवी अनुग्रह का प्रतिफल हाथों-हाथ प्राप्त करता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा ही गायत्री है। प्रज्ञा— अर्थात् दूरदर्शी विवेकशीलता, यही है मनुष्य का आराध्य। इस दिशा में होने वाली प्रगति से इसी जीवन में स्वर्ग और मुक्ति के रसास्वादन का लाभ मिलता है।
भविष्य निर्धारण की आराधना के निमित्त इस अवधि में स्वाध्याय, सत्संग और अन्तर्मुखी चिन्तन मनन के चार प्रयोजनों में निरत रहना पड़ता है। नित्यकर्म उपासना के अतिरिक्त जो भी समय खाली मिले उसमें उन्हीं चार प्रयोजनों में मन को लगाये रहना पड़ता है। इन चारों का लक्ष्य एक ही है—परिष्कार एवं उज्ज्वल भविष्य का योजनाबद्ध निर्धारण। इसके लिए आत्म निरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म निर्माण एवं आत्म विकास के चार प्रसंगों पर गम्भीरतापूर्वक समुद्र मंथन जैसा आत्म चिन्तन करते रहना होता है ताकि ईश्वर प्रदत्त अलभ्य उपहार-मनुष्य जन्म का सही उपयोग सम्भव हो सके। इसके लिए शरीर निर्वाह एवं परिवार पोषण की तरह ही परमार्थ प्रयोजनों को महत्व देना होता है। आत्म कल्याण और लोक मंगल की समन्वित जीवनचर्या का निर्धारण एवं सतत् अभ्यास ही आराधना है।
परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर उसके साथ तादात्म्य होना उपासना है। जीवन को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने वाली सुसंस्कारिता का अवधारण साधना है। लोक मंगल को परमार्थ और उनके सहारे अपनी सत्प्रवृत्तियों का सम्वर्धन ही आराधना है। उपासना परमात्मा की, साधना अन्तरात्मा की और आराधना विश्वात्मा की की जाती है। कल्प काल में बहिर्मुखी माया प्रपंच से अवकाश प्राप्त किया जाता है और उस अवधि में अन्तर्मुखी रह कर अन्तर्जगत का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस दिशा में परिवर्तन के लिए नियोजित आत्म साधना जितनी भावपूर्ण एवं गम्भीर होगी, उतना ही इस कल्प साधना का प्रत्यक्ष वरदान उपलब्ध होगा।
Write Your Comments Here:
- अध्यात्म क्षेत्र की उच्चस्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग
- कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
- साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलम्बन
- आन्तरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता
- कर्मफल की सुनिश्चतता : एक महत्वपूर्ण तथ्य
- दुष्कृतों के अवरोधों को हटाने की साहसिकता उभरे
- पापों का प्रतिफल और प्रायश्चित-शास्त्र अभिमत
- समस्त व्याधियों का निराकरण— आध्यात्म उपचार से
- प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
- हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
- क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
- कल्पकाल की आहार साधना
- आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
- अन्तर्मुखी प्रवृत्ति और निरन्तर आत्म-दर्शन
- जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
- आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन
- कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं
- कल्पकाल की अति फलदायी ऐच्छिक साधनायें
- आहार एवं औषधिकल्प के मूल सिद्धांत एवं व्यावहारिक स्वरूप
- आहार सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियां एवं उनका निवारण
- कल्प के पूर्व कुछ अनिवार्य ज्ञातव्य
- कल्प चिकित्सा की पात्रता के सम्बन्ध में महर्षि चरक का मत
- विभिन्न प्रकार के कल्प प्रयोग
- कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार