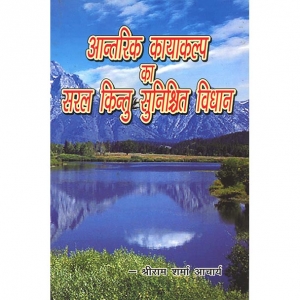आन्तरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिश्चित विधान 
हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
Read Scan Versionदूध, शाक, फल आदि बहुत देर तक यथा स्थिति में नहीं रखे जा सकते इसलिए अधिक मात्रा में होने पर उन्हें बेचकर रुपया बना लेते हैं। यह रुपया सुरक्षित रहता है, आवश्यकतानुसार उसके बदले दूध, शाक, फल अथवा दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इसी प्रकार दुष्कर्म घटनाक्रम के रूप में विस्तृत एवं सामयिक होने के कारण उन्हें पीछे अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए अन्तःचेतना ‘संस्कारों’ के रूप में सुरक्षित रख लेती है। यह संस्कार ही व्यक्तित्व का मूलभूत आधार होते हैं, इन्हीं के आधार पर गुण, कर्म एवं स्वभाव की विशेषताएं पूर्व संचित पूंजी के रूप में साथ बनी रहती है। यों सामयिक कमाई भी इसमें जुड़ती है और संचित संस्कार सम्पदा के प्रभाव को न्यूनाधिक करती रहती है।
मनुष्य जीवन की प्रमुख समस्याओं के कारण बाह्य परिस्थितियों में ढूंढ़ने की प्रचलित परम्परा को अपूर्ण ठहराया और अमान्य किया जा रहा है। व्यक्तित्व के अन्तराल में जमी हुई हठीली कुसंस्कार सम्पदा ही कठपुतली की तरह मनुष्य को त्रस्त किये रहती है, जब तक उसे बाहर न निकाल लिया जाय तब तक वह संकट दूर नहीं होता। आंख में तिनका और कान में मच्छर घुस जाय तो बेचैनी उत्पन्न होगी और वह तब तक बनी ही रहेगी, जब तक कि उन्हें निकाल न दिया जाय। पाप कृत्यों के बारे में भी यही बात है। वे बन पड़ें तो उन्हें प्रायश्चित के द्वारा निकाल बाहर करना ही एक मात्र उपाय है।
प्रमुख प्रश्न उन दुष्कर्मों का है जो भूतकाल में बन पड़े हैं और जिनके लिए आत्मा कचोटती और धिक्कारती है। वस्तुतः यह आत्म–प्रताड़ना ही शारीरिक, मानसिक रोगों को उत्पन्न करती रहती है। उसी उद्विग्नता में मन चंचल बना रहता है। न उपासना में लगता है, न सत्कर्मों में। इस कांटे को निकालना ही चाहिए। भोजन के साथ मक्खी पेट में चली गई तो उलटी कर देना ही एकमात्र उपाय है। भूतकाल में बन पड़े पापों का प्रायश्चित करके ही उनका शमन समाधान किया जा सकता है।
प्रायश्चित के चार चरण हैं—प्रथम दो पूर्वार्ध है, अन्तिम दो उत्तरार्ध—
जीवन भर के दुष्कर्मों की सूची बनाकर उनके द्वारा दूसरों को पहुंची हानि का स्वरूप समझना।
दुष्कर्मों का चिंतन कर आत्म-विश्लेषण करना, उन्हें न दोहराने का संकल्प एवं विज्ञजनों के समक्ष उनका प्रकटीकरण करते हुए प्रायश्चित का संकल्प लेना।
पश्चाताप के प्रतीक रूप में व्रत, उपवास, जप, अनुष्ठान आदि कृत्य करना।
व्यक्ति अथवा समाज को जो हानि पहुंची हो, उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए यथा सम्भव अधिकतम प्रयत्न करना।
पाप कर्म इसलिए बनते और बढ़ते रहते हैं कि कर्त्ता उनके द्वारा होने वाली हानियों पर ध्यान नहीं देता। उन्हें अन्य लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य क्रिया-प्रक्रिया मान लेता है। बाद में वे अभ्यास बन जाते हैं। धन, अधिकार, आतंक के उपयोग से उसे कई लाभ मिलने लगते हैं तो उनका आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है। कुमार्ग से विरत होने का यही मार्ग है कि उस मार्ग पर चलने वाले को उसकी हानियां स्वयं दृष्टिगोचर हों और प्रतीत हो कि इस दिशा में चलकर वह अब तक अपना तथा दूसरों का कितना अहित कर चुका। यही गतिविधियां जारी रहीं तो और भी कितनी हानि हो सकती है।
दुष्कर्मों, दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं से दूसरों का अहित और अपना हित होने की बात सोची जाती है, पर वस्तुस्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। कुमार्ग की कंटीली राह पर चलने से अपने ही पैर कांटों में बिंधते, अपने ही अंग छिलते और कपड़े फटते हैं। झाड़ियों को भी कुछ हानि होगी, पर इससे क्या? घाटे में तो अपने को ही रहना पड़ा। अपना मस्तिष्क विकृत होने से प्रगति के रचनात्मक कार्यों में लग सकने वाली शक्ति नष्ट हुई। अनावश्यक गर्मी के बढ़ने से यह बहुमूल्य यंत्र विकृत हुआ। शारीरिक और मानसिक रोगों की बाढ़ आई, मनःस्थिति गड़बड़ाने से क्रिया-कलाप उल्टे हुए और विपरीत परिस्थितियों की बाढ़ आ गई। हर दृष्टि से यह अपना ही अहित है। अस्तु बुद्धिमत्ता इसी में है कि सन्मार्ग पर चला जाय, सत्प्रवृत्तियों को अपनाया जाय और अन्तःकरण को सद्भावनाओं से भरा-पूरा रखा जाय।
इस प्रकार के चिंतन से ही वह विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण दुष्कर्मों के प्रति भीतर से घृणा उपजती है, पश्चात्ताप होता है। यही वे आधार हैं जिनके सहारे भविष्य में वैसा न होने की आशा की जा सकती है। अन्यथा, कारणवश उपजा सदाचरण का उत्साह, श्मशान-वैराग्य की तरह हो जायेगा और फिर उसी पुराने ढर्रे पर गाड़ी के पहिये लुढ़कने लगेंगे। प्रथम चरण में पश्चात्ताप की उपयोगिता इसी दृष्टि से है कि अन्तःकरण में अनाचार विरोधी प्रतिक्रिया इतनी उग्र रूप से उभरे कि भविष्य में उसी प्रकार के अनाचरण की गुंजाइश ही शेष न रह जाय।
दूसरा चरण मन की गांठें खोल देने का है। इसमें दूसरों का नहीं अपना ही लाभ है। अनैतिक दुराव के कारण मन की भीतरी परतों में एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियां बनती हैं। उनसे केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोग भी उठ खड़े होते हैं।
प्रकटीकरण के साथ-साथ उन दुष्कर्मों के प्रति लज्जित और दुःखी होने की वृत्ति का उभरना ‘पश्चात्ताप’ है। पश्चात्ताप में भविष्य में वैसा न करने का संकल्प भी रहता है अन्यथा ‘कह देने और करने लगने’ से तो बात ही क्या बनेगी। निश्चय किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार के पाप बन पड़े हैं वैसे अथवा अन्य प्रकार के दुष्कर्मों का साहसपूर्वक परित्याग किया जा रहा है। भविष्य में पवित्र और परिष्कृत जीवन ही जीना है। ऊपर से ही लीपापोती न की जा रही हो। अन्यथा पाप की जड़े जहां की तहां बनी रहेंगी। वे अवसर पाते ही फिर फलेंगी-फूलेंगी और पुनरावृत्ति होती रहेगी।
पश्चात्ताप का स्वरूप है—सच्चे मन से दुःखी होना। भूल की भयंकरता का अनुभव करना और भविष्य में इस प्रकार के आचरण न करने के लिए संकल्प करना और उसे कठोरतापूर्वक निवाहना। इतना कर चुकने पर ही प्रायश्चित की यथार्थता सामने आती है। पाप के प्रकटीकरण से कई लाभ होते हैं। मन के भीतर जो दुराव की गांठें बंधी रहती हैं वे खुलती हैं। मनोविज्ञान शास्त्र का सुनिश्चित मत है कि मनोविकारों के, दुष्कर्मों के दुराव से मानसिक ग्रन्थियां बनती हैं और वे अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों से उसके जीवन के घटनाक्रम को विस्तारपूर्वक बताने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। इसमें अप्रकट दुरावों का यदि प्रकटीकरण हो गया तो रोग का निराकरण सरल हो जाता है।
योऽन्यथा संतमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते ।
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ।।
—मनुस्मृति
जो अपनी वस्तुस्थिति को छिपाता है, जैसा कुछ है उससे भिन्न प्रकार को प्रकट करता है वह चोर, आत्महत्यारा और पापी कहलाता है।
कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवर्द्धते ।
स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धर्मविद्धयो निवेदयेत् ।।
तेहि पापे कृते वेद्या हन्तारश्वैव पाप्मनाम् ।
व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धिमन्तो रुजापहाः ।।
—पाराश स्मृति
पाप कर्म बन पड़ने पर उसे छिपाना नहीं चाहिए। छिपाने से वह बहुत बढ़ता है। पाप छोटा हो या बड़ा उसे किसी धर्मज्ञ से प्रकट अवश्य कर देना चाहिए। इस प्रकार उसे प्रकट कर देने से पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे चिकित्सा करा लेने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रकटीकरण की महत्ता बताते हुए शास्त्र कहता है—
तस्मात् पापं गूहेत गुह्यमानं विवर्धयेत् ।
कृत्वा तत् साधुष्वखमेयं ते तत् शमयन्त्युत ।।
—महा. अनु.
अतः अपने पाप को न छिपायें। छिपाया हुआ पाप बढ़ता है। यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे साधु पुरुषों से कह देना चाहिए वे उसकी शांति कर देते हैं।
प्रकटीकरण के उपरान्त प्रतीकात्मक दण्ड व्यवस्था का चरण है। यह सांकेतिक है। बच्चे के गलती करने पर उसे कान पकड़ने, कोने में खड़ा होने, बैठक आदि करने के हल्के दण्ड दिये जाते हैं, यह लाक्षणिक हैं। उनका महत्व इतना भर है कि इस प्रताड़ना की स्मृति, गलती की भयंकरता और उसकी पुनरावृत्ति न करने की आवश्यकता की छाप अन्तःचेतना पर अधिक अच्छी तरह छोड़ सके, वास्तविक समाधान तो कान पकड़ना—यदि यही क्रम चलने लगे तो बात उपहासास्पद बन जायगी। यदि बच्चा किसी की कापी चुरा लाया है तो कान पकड़ने भर से उसका प्रायश्चित नहीं हुआ। वह तो स्मृति को झकझोरना भर है। जिसकी कापी चुराई गई थी, उसकी क्षति पूर्ति इतने भर से कहां हुई? उसकी तो कापी वापिस मिलनी चाहिए, जो हानि हुई उसकी भरपाई का प्रबन्ध होना चाहिए। प्रायश्चित का असली भाग वही है जिसमें ऋण मोचन किया जाता है।
अनैतिक दुरावों के प्रकटीकरण में खतरा भी है कि ओछे व्यक्ति उन जानकारियों का अनुचित प्रयोग करने बदनामी करने तथा हानि पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अस्तु निस्संदेह इस प्रकटीकरण के लिए ऐसे सत्पात्रों को ही चुनना चाहिए जिसकी उदारता एवं दूरदर्शिता असंदिग्ध हो। चिकित्सक के आगे रोगी को अपने यौन रोगों की वस्तुस्थिति बतानी पड़ती है। उदार चिकित्सक उन कारणों को प्रकट करते नहीं फिरते, जिनकी वजह से वह रोग उत्पन्न हुए। उनका दृष्टिकोण रोगी की कष्ट निवृत्ति भर होता है। ऐसे ही उदार चेतना एवं उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ व्यक्ति ही इस योग्य होते हैं जिनके सामने मन की दुराव ग्रन्थियां खोली जा सकें।
ईसाई धर्म में प्रवेश करने वाले को ‘वपतिस्मा’ लेना पड़ता है। उस संस्कार के समय मनुष्य को अब तक के अपने पाप पादरी के सम्मुख एकान्त में कहने होते हैं। उस धर्म में मृत्यु के समय भी यही करने की धर्म परम्परा है। मरणासन्न के पास पादरी पहुंचता है। उस समय अन्य सभी लोग चले जाते हैं। मात्र पादरी और मरणासन्न व्यक्ति ही रहते हैं। वह व्यक्ति अपने पापों को पादरी के सामने प्रकट करता है। इस प्रकार उसके मन पर चढ़ा भार हल्का हो जाता है। पादरी शांति-सद्गति की प्रार्थना करता और रोगी को आश्वस्त करके महाप्रयाण के लिए विदा करता है। वपतिस्मा और मरणकाल में इस स्वीकारोक्ति को—‘कन्फैशन’ को अत्यन्त पवित्र और आवश्यक माना गया है। मनःशास्त्र के अनुसार यह प्रथा नितान्त श्रेयस्कर ठहराई गई है।
प्रायश्चित प्रकटीकरण को एक अति महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अनैतिक कृत्यों के दुराव को कभी किसी के सामने प्रकट न किया जाय तो मनःक्षेत्र में वह उर्वरता उत्पन्न न हो सकेगी जिनसे आध्यात्मिक सद्गुणों का अभिवर्धन सम्भव होता है।
Write Your Comments Here:
- अध्यात्म क्षेत्र की उच्चस्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग
- कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
- साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलम्बन
- आन्तरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता
- कर्मफल की सुनिश्चतता : एक महत्वपूर्ण तथ्य
- दुष्कृतों के अवरोधों को हटाने की साहसिकता उभरे
- पापों का प्रतिफल और प्रायश्चित-शास्त्र अभिमत
- समस्त व्याधियों का निराकरण— आध्यात्म उपचार से
- प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
- हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
- क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
- कल्पकाल की आहार साधना
- आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
- अन्तर्मुखी प्रवृत्ति और निरन्तर आत्म-दर्शन
- जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
- आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन
- कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं
- कल्पकाल की अति फलदायी ऐच्छिक साधनायें
- आहार एवं औषधिकल्प के मूल सिद्धांत एवं व्यावहारिक स्वरूप
- आहार सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियां एवं उनका निवारण
- कल्प के पूर्व कुछ अनिवार्य ज्ञातव्य
- कल्प चिकित्सा की पात्रता के सम्बन्ध में महर्षि चरक का मत
- विभिन्न प्रकार के कल्प प्रयोग
- कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार