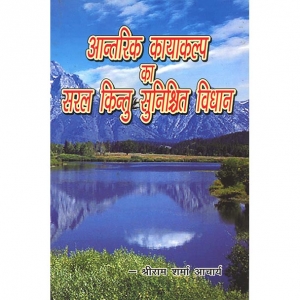आन्तरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिश्चित विधान 
जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
Read Scan Version‘हर दिन नया जन्म और हर रात नया मरण’—मानकर चलने से जीवन सम्पदा के सदुपयोग के लिए अन्तः प्रेरणा उभरती है। इसलिए हर साधक को विशेषतया कल्प प्रक्रिया में निरत श्रेयार्थियों को इस साधना को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। यह साधना वस्तुतः जीवन को एक नयी दिशा देने वाली साधना है। प्रातःकाल नींद खुलते ही नया जन्म होने की कल्पना जगाई जाय, भावना उभारी जाय। साथ ही यह भी सोचा जाय कि मात्र एक दिन के लिए मिले इस सुयोग-सौभाग्य का श्रेष्ठतम सदुपयोग किस प्रकार किया जाय। कुछ समय इसी सोच विचार में लगाने के उपरान्त बिस्तर छोड़कर उठना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए जाना चाहिए।
ठीक इसी प्रकार रात्रि को सोते समय यह विचार करना चाहिए कि निद्रा एक प्रकार की मृत्यु है। अब मरण की गोद में जाया जा रहा है। मृत्यु के उपरान्त प्राणी ईश्वर के दरबार में पहुंचता है। पहुंचने ही तत्काल पूछताछ होती है। इस पूछताछ का एक ही विषय होता है—‘‘सुर दुर्लभ मनुश्य जीवन किस प्रयोजन के लिए दिया गया था? उसका उपयोग किस प्रकार किया गया? इसका विवरण दिया जाय।’’ इस विवरण को शानदार ढंग से सिर उठाकर दिया जा सके ताकि उससे परलोक का अधिष्ठाता संतोष व्यक्त कर सके, अगली बार कुछ बड़ा पद उत्तरदायित्व सौंपने का विचार कर सके। यही है वह भविष्य-चिन्तन जिसे रात्रि को सोते समय तब तक करते ही रहना चाहिए जब तक कि निद्रा स्वयं आकर अपने अंचल से ढक न ले।
उठते समय की उपरोक्त साधना को ‘आत्मबोध’ और सोते समय वाले चिन्तन को ‘तत्वबोध’ कहा गया है। यह दोनों देखने, कहने, सुनने एवं करने में अत्यन्त साधारण जैसी लगती हैं किन्तु यदि चिह्न पूजा की तरह उसकी लकीर न पीटी जाय और गम्भीरतापूर्वक उन विचारणाओं की परिणति एवं फलश्रुति पर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि इस बीज का विकास-विस्तार विशालकाय वट वृक्ष के रूप में होता है। चिनगारी तनिक-सी होती है किन्तु उसे ईंधन की सुविधा मिल सके तो उसे प्रचण्ड दावानल बनते और योजनों लम्बा वन प्रदेश उदरस्थ करते देर नहीं लगती। आंख से न दीख पड़ने वाला, बाल की नोंक से भी कम विस्तार वाला शुक्राणु जब नौ महीने जितने स्वल्प काल में एक अच्छा खासा शिशु बनकर प्रकट होता है तो कोई कारण नहीं कि उपरोक्त विचार द्वय समुचित परिपोषण पाने पर जीवन को देवत्व से लपेट देने वाले वरदान सौभाग्य के रूप में प्रकट विकसित न हो सकें।
जन्म के उपरान्त जीवन सम्पदा के उपयोग का अवसर मिलता है और मरण के उपरान्त ईश्वर की न्याय-दीर्घा में खड़े होकर कृत्यों का परिणाम भुगतने के लिए विवश होना पड़ता ह। इन दोनों का सामना न करना पड़े, ऐसा बचाव किसी भी मनुष्य शरीरधारी के लिए सम्भव नहीं। अस्तु, उसका सामना करने के लिए मनोभूमि बनाने एवं तैयारी करने में ही बुद्धिमत्ता है। चिनतन-चेतना के इस संदर्भ में उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए वरन् जो अवश्यम्भावी है उसके लिए समय रहते जागरूकता बरतने एवं तत्परता अपनाने में ही दूरदर्शिता है।
इस तथ्य को जितनी गम्भीरतापूर्वक समझा जाय उतना ही अच्छा है कि उपलब्ध मनुष्य जीवन, ईश्वर का सर्वोपरि उपहार है। उसमें आत्मोत्कर्ष की समस्त सम्भावनायें भरी पड़ी हैं। साथ ही ईश्वर को प्रसन्न करने तथा उस अनुकम्पा के आधार पर कुछ पाने का यही ठीक अवसर है। इसे महत्वहीन न समझा जाय। उसे भार की तरह न ढोया जाय। इस अलभ्य सौभाग्य को अस्त-व्यस्त प्रयोजनों में न गंवाया जाय। बुद्धिमत्ता इसी में है कि संयोगवश आरम्भ में उगे कल्प-वृक्ष को ठीक तरह सींचा-पोसा जाय, प्रतिकूलताओं से बचाया जाय और उसे विकसित स्थिति तक पहुंचाया जाय जिससे उसकी सुखद छाया में बैठने और अभीष्ट वरदान पाने का सौभाग्य बरसने लगे। अज्ञानग्रस्त इस अलभ्य अवसर का न मूल्यांकन कर पाते हैं और न उसके सदुपयोग की कोई योजना-व्यवस्था बनाते हैं। फलतः अनाड़ी के हाथ पड़े हुए हीरक हार की तरह उसके साथ खिलवाड़ होती और धागे टूटने, मनके बिखरने जैसी विडम्बना बनती रहती है। इससे बड़ी दुर्भाग्य भरी दुर्घटना और नहीं हो सकती कि जीवन का महत्व न समझा जा सके उसका मूल्यांकन न बन पड़े और किसी प्रकार मौत के दिन पूरे कर लेने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले न पड़े। पेट-प्रजनन में व्यस्त रहना तो तुच्छ प्राणियों को क्रियाशील रखने वाला प्रकृति का हण्टर भर है। वह तो हर योनि में पड़ता ही रहा है, भविष्य में जन्म लेना पड़े तो उनमें भी यह सटापट बरसेगा ही। मानवी बुद्धिमत्ता की सार्थकता इसमें है कि वह इस अलभ्य अवसर का सौभाग्य मय सदुपयोग समझें। इस निष्कर्ष पर पहुंचाकर उस मार्ग पर चलायें जिसके आधार पर वर्तमान को समुन्नत और भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकना सम्भव हो सकता है। इसके लिए उपयुक्त दिशाधारा का सुनिश्चित निर्धारण बन पड़े तो ही प्रस्तुत सौभाग्य से लाभान्वित हो सकना सम्भव है। देखना यही है कि प्रस्तुत कल्प साधना को जीवन में एक महान् मोड़ दे सकने वाली प्रखरता से सम्पन्न बनाया जा सका या नहीं।
साधकों को अनुभव करना चाहिए कि वे इस अवधि में माता के गर्भ में निवास कर रहे हैं और ऐसा आवश्यक पोषण प्राप्त कर रहे हैं जिसके सहारे जन्म लेने के उपरान्त समूचे जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग कर सकने में समर्थ हो सकें। गुरु-गृह को भी माता के गर्भ के सदृश्य माना गया है। साधक की इन दिनों मान्यता ऐसी ही होनी चाहिए। ऊषाकाल, रात्रि की विदाई और दिनमान की अगवानी करता है। कल्प साधना की अवधि में ऐसी ही अनुभूति होनी चाहिए कि नर पशु का स्तर त्यागने और देव स्तर में प्रवेश करने का यही ऊषाकाल है। इन्हीं क्षणों में महान् परिवर्तन की सम्भावना बन रही है। सघन संव्याप्त तमिस्रा का पलायन और समूचे आकाश में प्रभात का प्रकाश वितरण सचमुच ही आश्चर्य है। इतने थोड़े क्षणों में इतना महान् परिवर्तन देखते हुए लगता है ऊषाकाल की प्रभात बेला कितनी अद्भुत, कितनी सशक्त एवं कितनी सौभाग्यशाली है, इसी प्रकार चान्द्रायण तपश्चर्या की भूमिका भी ऐसी ही होनी चाहिए जिसे कर्त्ता का अभिनव भाग्योदय कहकर शेष सारा जीवन सराहा और स्मरण रखा जा सके।
पर यह सम्भव तभी है जब साधक इन दिनों अपनी भाव भूमिका को गतिशील रखे और पराक्रम की चरम सीमा तक पहुंचे। यों माता भी भ्रूण को बहुत कुछ देती है, पर उसे भ्रूण के निजी पुरुषार्थ की तुलना में नगण्य ही कहा जा सकता है। शरीर शास्त्री जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु आत्मविकास के लिए जितना पराक्रम करता है उतना ही वह जन्म लेने के उपरान्त भी जारी रख सके तो उसे देव-मानवों जैसी महानता उपलब्ध हो सकती है। भ्रूण जब परिपक्व हो जाता है तो उदर दरी से बाहर निकलने में उसी को चक्रव्यूह बेधने जैसा पराक्रम करना पड़ता है। प्रसव पीड़ा उसी व्याकुल प्रयत्नशीलता की परिणति है। यदि भ्रूण दुर्बल है तो उसे पेट चीरकर निकालना पड़ेगा। स्वाभाविक प्रसव सम्भव न हो सकेगा। अण्डे को मुर्गी देती तो है, पर उसके भीतर भरे कलल में उसका जो निजी समुद्र मन्थन चलता है उसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है। पका अण्डा जब फूटने को होता है तो उसकी सारी भूमिका भीतर वाले चूजे को ही निभानी पड़ती है। फूटने के समय अण्डा थरथराता है, उसमें पतली दरार पड़ती है, दरार तेजी से चौड़ी होती है और बच्चा उछलकर ऊपर आ जाता है। यह पुरुषार्थ न बन पड़े तो अण्डा सड़ेगा और उससे बच्चा निकलने की बात किसी भी प्रकार बनेगी नहीं। कल्प तपश्चर्या के साधकों को दैवी अनुग्रह की भी कमी नहीं रहने वाली। पर उड़ने भर से ही अभीष्ट प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है। भ्रूण एवं चूजे की तरह आवरण को तोड़कर बाहर निकलने के लिए पराक्रम तो उसका ही प्रमुख रहेगा। उस उक्ति में परिपूर्ण सचाई भरी हुई है जिसमें कहा गया है कि ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं।
जीवन अपने आप में पूर्ण है। वह पूर्ण से उत्पन्न हुआ है और पूर्णता से परिपूर्ण है अंगार और चिनगारी में आकार का भेद तो है पर गुण धर्म का नहीं। परमात्मा विभु है, आत्मा लघु। यह आकार भेद हुआ। तात्विक दृष्टि से दोनों में समानता है। इसलिए ‘शिवोऽहम्-सच्चिदानन्दोऽहम्’ के रूप में उस तात्विक एकता का उद्बोधन कराया जाता है। इस तथ्य के रहते मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है? वह दीन दुर्बल क्यों रहता है? शोक सन्ताप क्यों सहता है? प्रगति प्रक्रिया से वंचित रहने का क्या कारण है? इस दुर्गुण के रहते तो कुबेर का खजाना खाली हो सकता है। रावण जैसा समर्थ भी सपरिवार धराशायी हो सकता है। भस्मासुर, वृत्रासुर, हिरण्याक्ष जैसे दुर्दान्त दैत्य बेमौत मारे गये। इस विनाशलीला में उनके अपने दोष-दुर्गुणों की भूमिका ही प्रधान थीं।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु असंयम है। सामर्थ्यों का अपव्यय, दुरुपयोग ही असंयम है। शक्ति तथा सम्पन्नता का लाभ तभी मिलता है जब उसका सदुपयोग बन पड़े। दुरुपयोग होने पर तो अमृत भी विष बन जाता है। माचिस जैसी छोटी एवं उपयोगी वस्तु अपना तथा पड़ौसियों का घर-बार भस्म कर सकती है। ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्यों का सदुपयोग कर सकने की सूझ-बूझ एवं संकल्प शक्ति को ही मर्यादा पालन एवं संयमशीलता कहते हैं। इसी का अभ्यास करने के लिए कई प्रकार की तप साधनायें करनी पड़ती हैं। कल्प से जुड़ी तप साधनाओं में भी उस प्रखरता को उभारना एक बड़ा उद्देश्य है जो मानवी शक्ति को अभ्यस्त अपव्यय से बलपूर्वक बचाती और दबाव देकर उसे सत्प्रयोजनों में निरत करती है।
संयम साधना के चार प्रमुख आधार हैं—
(1) इन्द्रिय संयम,
(2) अर्थ संयम,
(3) समय संयम,
(4) विचार संयम।
वस्तुतः यही चार शक्तियां जीवन सत्ता के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्हीं का संचय-सम्वर्धन करके कोई सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान बनता है। बाहरी शक्तियां तो अस्थिर भी हो सकती हैं और प्रयोक्ता की अदूरदर्शिता के कारण कई बार उसी के लिए घातक बनती हैं।
प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वालों में से प्रत्येक को अपनी समर्थता को अपव्यय से बचाकर अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना पड़ता है। कल्प साधकों को भी साधना काम में तो उपरोक्त चारों प्रकार के संयम विवश होकर बरतने ही पड़ते हैं। किन्तु इसी अवधि में यह निर्णय भी करना होता है कि साधना काल समाप्त होने के उपरांत संयम साधना को जीवन चर्या का अविच्छिन्न अंग बनाकर रहेंगे। वस्तुतः भावी जीवन की तैयारी का निर्धारण ही इस कल्प साधना का सही एवं एकमात्र उद्देश्य है। थोड़े दिनों तो संयमी-तपस्वी बन कर रहा जाय और कल्प सूत्र समाप्त होते ही पुरानी बेतुकी आदतों में जुटा पड़ा जाय तो स्नान करके फिर कीचड़ लपेट लेने जैसी एक विडम्बना ही तो हुई।
इन्द्रिय संयम में जिह्वा एवं जननेन्द्रिय पर छाये रहने वाले चटोरेपन का शमन करना पड़ता है। जीभ की चटोरी आदतों के कारण स्वाद के नाम पर अभक्ष्य खाने से अनावश्यक मात्रा में पेट पर बोझा लदता है। फलतः अत्याचार पीड़ित पेट में अपच रहने लगता है और चित्र-विचित्र नाम-रूपों वाली बीमारियों से शरीर संत्रस्त रहने लगता है। दुर्बलता और अकाल मृत्यु इसी असंयम की परिणति है। उत्तेजक, गरिष्ठ एवं भुने-तले पदार्थ न केवल दुष्पाच्य होते हैं वरन् मन को चंचल, दुर्बल, दूषित एवं कुमार्गगामी भी बनाते हैं। मनोरोग ग्रस्त व्यक्ति किस प्रकार संकट सहते और त्रास देते हैं यह सर्वविदित है। इन मनोरोगों का एक बहुत बड़ा कारण अभक्ष्य भी होता है। चटोरेपन से मुक्ति पाने के लिए समय-समय पर लम्बे अस्वाद व्रत करने होते हैं और सामान्य आहार क्रम में सात्विक पदार्थों को न्यूनतम मात्रा में ही अग्नि संस्कार कर उपयोग में लाते हैं। इसी का एक स्वरूप, भले न्यूनतम ही सही, कल्प साधना में बनाया गया है।
जीभ का दूसरा संयम संयत वचन बोलना है। संक्षेप में सारगर्भित, सदाशयतापूर्ण, शालीनता समर्थक, नम्रता युक्त मधुर वाणी का अभ्यास तप कहलाता है। सत्य बोलने के अन्तर्गत बात को ज्यों का त्यों कह देना ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ वे सारी विशेषतायें भी जुड़ी रहनी चाहिए जिन्हें अपनाने से वचन में शालीनता की झांकी मिलती है। मौन इसी अभ्यास के लिए अपनाना पड़ता है। प्रायः यहां मौन रहने का विधान इस साधना में इसी कारण है।
इन्द्रियों में जिह्वा और कामेन्द्रिय प्रधान हैं। उन्हें साध लेने से मन समेत अन्य इन्द्रियां सरलतापूर्वक सध जाती हैं। ब्रह्मचर्य का माहात्म्य सर्वविदित है। ओजस् को जितनी कम मात्रा में खर्च किया जाय, उतना ही नर और नारी दोनों का हित है। स्खलन से दाद खुजाने जैसी क्षणिक गुदगुदी भले ही मिलती हो, जीवनी शक्ति का भण्डार तो घटता ही है। यौनाचार की तरह ही कामुकता का वातावरण, चिन्तन, दृष्टिकोण भी उस अदृश्य शक्ति का विनाश करता है जिसे रचनात्मक प्रयोजनों में प्रयुक्त करके अनेकानेक उपयोगी सफलताएं उपलब्ध कर सकना सम्भव है। यों इन्द्रियों में आंख, कान, नाक आदि की भी गणना है, पर उनके असंयम उतने नहीं होते जितने चटोरेपन और कामुकता के। असंयम वार्तालाप प्रत्यक्षतः कितने दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, यह सर्वविदित है। उस कारण ओजस् शक्ति का क्षरण होने एवं प्रतिभा भण्डार में कमी पड़ने की हानि को भी जाना जा सकता है। वाणी का संयम ही है जिसके कारण ईश्वर प्रार्थना में बल आता है, मंत्राराधन सफल होता है और परामर्श प्रवचनों के प्रभावी होने से लेकर शाप वरदान देने की सामर्थ्य तक का उद्भव होता है।
दूसरा संयम है—अर्थ संयम। दुर्व्यसन, ठाट-बाट, फैशन-शृंगार, प्रदर्शन, दर्प में जितना पैसा खर्च होता है इसे रोककर सत्प्रयोजनों में लगाया जा सके तो अपव्ययजन्य दोष-दुर्गुणों से बचने, दरिद्रता घटने तथा उपयोगी कार्यों के लिए कुछ साधन बचने जैसे कितने ही लाभ मिल सकते हैं। ‘सादा जीवन-उच्च विचार’ का सिद्धांत आध्यात्मिकता का, शालीनता का मेरुदण्ड है। उसका परित्याग करके विलासी, उच्छ्रंखलता अपनाई जाय तो अनायास ही व्यक्तित्व में अनेकानेक दोष-दुर्गुण घुस पड़ेंगे। इस विपत्ति से बचना हो तो अर्थ संयम बरतने में कठोरता अपनानी चाहिए। औसत भारतीय स्तर का निर्वाह पर्याप्त समझा जाना चाहिए। शेष बचत का ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसा परमार्थ परक उपयोग हो सकता है।
सन्तान की संख्या बढ़ाना, परिवार को आलसी-अकर्मण्य बनाकर एक व्यक्ति की आजीविका पर निर्भर कर देना भी प्रकारान्तर से अपव्यय बढ़ाना ही है। इन आधारों पर अर्थ संकट खड़ा करने में किसी भी दृष्टि से बुद्धिमानी नहीं है। परिवार छोटे रहें। हर सदस्य मितव्ययी एवं परिश्रमी बने तब उस अर्थ संकट से बचा जा सकता है जिससे आजकल हर व्यक्ति संत्रस्त है।
विवाह शादियों की धूमधाम में अनावश्यक खर्च करने जैसी कुरीतियां भी बरबादी का कारण बनी हुई हैं। उत्तराधिकार में बहुत कुछ छोड़ मरने, जो कमाया उसे सन्तान को ही देने की प्रवृत्ति ऐसी है जिसे प्रचलित होते हुए भी अनैतिक एवं अदूरदर्शितापूर्ण ही कहा जायगा। इन सभी अपव्ययों पर अंकुश लगाया जा सके तो वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन में अनेकों सत्प्रवृत्तियां पनपेंगी। नीतियुक्त उपार्जन और विवेकपूर्ण उपयोग का सिद्धांत यदि व्यावहारिक जीवन में अपनाया जा सके तो समझना चाहिए कि तपश्चर्या का एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत जीवन-क्रम में सम्मिलित हो गया और उसकी दूरगामी सत्परिणाम उपलब्ध होना सुनिश्चित है। यह एक श्रेष्ठ सत्परम्परा तो है ही, साथ ही साधनों का सीमित व्यय किये जाने पर उपलब्ध प्रकृति सम्पदा का लाभ उन अभावग्रस्तों को भी मिल जाता है जो सम्पन्नों द्वारा अनावश्यक अपव्यय किये जाने पर उनके हिस्से में आती ही नहीं या फिर दाम ऊंचे चढ़ जाने के कारण वे उन्हें खरीद ही नहीं सकते। सादगी सात्विकता की प्रतीक है। उसमें नम्रता की झलक है जिसे अपनाने पर सहज सज्जनता पनपती है और ईर्ष्या-द्वेष का एक बड़ा कारण कम होता है।
तीसरा संयम है—‘समय संयम’। समय को लोग ऐसे ही आलस्य प्रमाद में काटते रहते हैं। मन्दगति से अन्यमनस्क होकर बेगार भुगतने की तरह किये गये काम समय तो नष्ट करते ही हैं, मात्रा में भी स्वल्प एवं गुणवत्ता में भौंड़े, घटिया ही होते हैं। इस प्रकार समय उतना ही खर्च हो जाने पर भी उसका परिणाम घटिया स्तर का मिलता है। समय संयम का तात्पर्य है—एक क्षण भी अनावश्यक कामों में अथवा व्यर्थ-निरर्थक नष्ट न होने देना। हर मिनट को हीरे-मोती से तौलने योग्य बहुमूल्य मानना और उसे पूरी मुस्तैदी के साथ उपयोगी कार्यों में नियोजित रखे रहना। जो ऐसा कर पाते हैं, वे सामान्य लोगों की तुलना में उतने ही समय में कई गुना, कहीं अधिक महत्वपूर्ण सराहनीय स्तर का काम कर लेते हैं। थोड़ी-सी जागरूकता, तत्परता, तन्मयता का समावेश कर लेने से समय की आराधना बन पड़ती है और एक से एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सुयोग हस्तगत होता चलता है।
समय ही जीवन है। कौन कितना जिया, इसका मूल्यांकन वर्षों की गणना के नहीं किया जाना चाहिए। वरन् यह देखना चाहिए किसने कितनी तत्परता के साथ किस स्तर के कामों में अपना समय लगाया। इस कसौटी पर कम समय जीने वाले भी अपने क्रिया कृत्यों के आधार पर दीर्घजीवी कहे जा सकते हैं और निरर्थक समय गंवाते रहने वाले शत आयुष लोगों को भी अल्पकाल जीने वालों, अकाल मृत्यु मरने वालों में ही गिना जायेगा। आद्य शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिये। विवेकानन्द 36 वर्ष की आयु में दिवंगत हो गये। उतने समय में उनने महत्वपूर्ण स्तर के इतने काम कर लिए जिन्हें देखते हुए किसी शतायु से कम नहीं अधिक समय तक जीने वाला ही कहा जा सकता है।
रावण के सम्बन्ध में कथा है कि उसने काल को चारपाई की पाटी से बांध रखा था। उसी की अभ्यर्थना से उसने अनेक प्रकार की शक्तियां, सम्पदाएं उपलब्ध की थीं। काल को इन दिनों भी कलाई पर हाथ-घड़ी के रूप में बांधा जाता है। पर उनमें से कोई विरले ही यह समझते हैं कि इस उपकरण का उद्देश्य समय का ध्यान रखना, उसका सुनियोजित उपयोग करना है।
जिनने समय उथले कामों में अथवा आलस्य प्रमाद में बिताया, समझना चाहिए कि उन्होंने ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य सम्पदा को फुलझड़ी बनाकर जलाया। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि ईश्वरीय सम्पदा के रूप में मनुष्य को समय ही मिला है। उसके बदले में संसार के बाजार में कोई भी भली बुरी वस्तु खरीदी जा सकती है। पैसा भी प्रकारान्तर से समय श्रम का ही घनीभूत स्वरूप है। वैभव के समस्त साधन, स्वरूप वस्तुतः समय की कीमत पर ही खरीदे जाते हैं। जुआ, चोरी की तरह कोई बिना श्रम के ही किसी प्रकार की कमाई हस्तगत कर ले तो उसे अवांछनीय ही कहा जायेगा।
समय सम्पदा के बदले ही भौतिक सफलतायें अर्जित की जाती हैं और उसी के बदले आत्मिक क्षेत्र की विभूतियां उपलब्ध होती हैं। जिन्हें मौत के दिन पूरे नहीं करने हैं, जो जीवन का मूल्य समझते हैं और उससे कुछ महत्वपूर्ण उपलब्ध करना चाहते हैं, उन्हें यह तथ्य गांठ-बांध लेना चाहिए कि समय को ही जीवन समझें और दैनिक दिनचर्या में एक समूचे जीवन का कार्य निर्धारण बनाकर एक निश्चित नीति अपनायें। निरन्तर इस बात का ध्यान रखें कि कहीं समय सम्पदा का अपव्यय तो नहीं हो रहा है। अन्तिम सांस तक जीवन की हर घड़ी, पल का आदर्शवादिता का पक्षधर उपयोग होता रहे। ऐसी व्यवस्था बनाकर चलने वाले ही जीवन आनन्द लेने और गर्व से संतोष करते पाये जाते हैं।
चौथा संयम है-विचार संयम। विचार अदृश्य होते हैं। इसलिए आमतौर से उन्हें पदार्थ वैभव नहीं माना जाता और उन्हें उपयोगी प्रयोजनों में ही नियोजित किया जाता है, इसका किसी को ध्यान ही नहीं रहता। समझा जाना चाहिए कि विचार भी समय या धन की तरह एक सामर्थ्य है। उन्हीं के आधार पर कर्म की प्रेरणा मिलती है, साधन जुटते हैं और उत्थान-पतन का क्रम चलता है। वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, विशेषज्ञ जन्मजात रूप से किन्हीं आंतरिक विशेषताओं से सम्पन्न नहीं होते, मात्र अपने विचारों को अस्त–व्यस्त होने से रोककर उन्हें अभीष्ट प्रयोजनों में ही नियोजित किये रहते हैं। फलस्वरूप बिखराव को समेटने का यह कौशल उन्हें निश्चित क्षेत्र में प्रवीण-पारंगत बना देता है।
अध्यात्म क्षेत्र में बहुचर्चित ध्यान-धारणा में विचारों को एकाग्र करके लक्ष्य विशेष पर केन्द्रित करने का अभ्यास करना पड़ता है। यह एक उच्चस्तरीय कला-कौशल है।
किसी विषय में प्रवीण पारंगत होने के लिए उसके साथ अभिरुचि जोड़नी पड़ती है। साथ ही विचारों को आवारागर्दी में भटकने से रोककर उन्हें निर्धारित प्रयोजनों में कार्यरत रहने को अभ्यस्त करना होता है। इस प्रसंग में जिसे जितनी सफलता मिलेगी वह उसमें उतनी ही मूर्धन्य स्थिति प्राप्त करता चला जायेगा। महामानवों में से प्रत्येक ने विचारों को अभीष्ट लक्ष्य के साथ तत्परतापूर्वक जोड़े रहने की बुद्धिमत्ता अपनाई और उसी जागरूकता के आधार पर वे प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले गये।
कल्प एक प्रकार की तप साधना है। उसमें निर्धारित अवधि में तो उपरोक्त चारों संयम अपनाने ही होते हैं, साथ ही यह निश्चय निर्धारण भी करना होता है कि समाप्त होने के उपरांत भी वे इन्हें जीवनचर्या का अंग बनाकर रखेंगे। जिनने यह निश्चय किया और उसे व्रतपूर्वक निभाया, समझना चाहिए कि उनका भविष्य उज्ज्वल बनने में किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रह गया। व्रत साधना के दिनों में यही चिंतन-मनन करते रहना चाहिए—जीवन का किस प्रकार श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जा सकता है और महत्वपूर्ण कृतियां साथ लेकर परमेश्वर के दरबार में कैसे गर्वोन्नत मस्तक से जाया जा सकता है ?
Write Your Comments Here:
- अध्यात्म क्षेत्र की उच्चस्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग
- कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
- साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलम्बन
- आन्तरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता
- कर्मफल की सुनिश्चतता : एक महत्वपूर्ण तथ्य
- दुष्कृतों के अवरोधों को हटाने की साहसिकता उभरे
- पापों का प्रतिफल और प्रायश्चित-शास्त्र अभिमत
- समस्त व्याधियों का निराकरण— आध्यात्म उपचार से
- प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
- हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
- क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
- कल्पकाल की आहार साधना
- आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
- अन्तर्मुखी प्रवृत्ति और निरन्तर आत्म-दर्शन
- जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
- आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन
- कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं
- कल्पकाल की अति फलदायी ऐच्छिक साधनायें
- आहार एवं औषधिकल्प के मूल सिद्धांत एवं व्यावहारिक स्वरूप
- आहार सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियां एवं उनका निवारण
- कल्प के पूर्व कुछ अनिवार्य ज्ञातव्य
- कल्प चिकित्सा की पात्रता के सम्बन्ध में महर्षि चरक का मत
- विभिन्न प्रकार के कल्प प्रयोग
- कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार