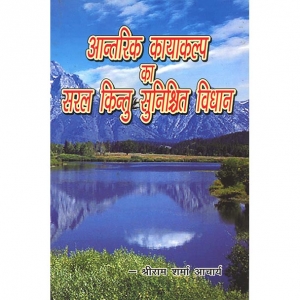आन्तरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिश्चित विधान 
कल्पकाल की आहार साधना
Read Scan Versionपरिस्थितियों को बदलना मनःस्थिति के हाथ में है। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का रोना तो भीरू, कायर, जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ व्यक्ति रोते हैं। परिस्थितियों का सम्बन्ध बाह्य व्यक्तियों तथा सुविधाओं पर जितना निर्भर माना जाता है, उससे कहीं अधिक व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर है। यदि व्यक्तित्व में बहिरंग को बदल डालने-अपने परिकर का कायाकल्प कर डालने की सामर्थ्य है तो कोई भी व्यवधान प्रगति को नहीं रोक सकता। यह तो मन का प्रमाद व अचेतन का ढर्रा है जो, ‘‘जैसा कुछ है वैसा ही चलने दो’’ की स्थिति के लिए विवश करता है। मनुष्य एक जीता जागता चुम्बक है जो अपने स्तर के अनुरूप परामर्श, वातावरण सहयोग, साधन चुपके-चुपके खींचता रहता है। उसके आस-पास वैसा ही परिकर जुट जाता है जैसी कि मनःस्थिति होती है। चोर, जेबकट, सन्त, सज्जन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, आलसी, दरिद्र, दुर्व्यसनी अपने-अपने ढंग का समाज, अपने अनुकूल परिस्थितियां अपने चारों ओर बना लेते हैं। परिकर व साधन के समन्वय को परिस्थिति कहते हैं। अपवाद तो कहीं न कहीं बनते हैं। उत्थान और पतन के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी होता है। इस कथन को बार-बार समझना, आत्मसात कर लेना चाहिए।
इस केन्द्र स्थली मनःसंस्थान को कैसे पवित्र, परिष्कृत बनाया जाय। इसके दो उपाय पहले ही बताये गये हैं। एक चिंतन-मनन द्वारा अन्तःप्रेरणा उभारने और तदनुरूप जीवन की दिशा-धारा को बदलने का भावनात्मक उपाय और दूसरा-साधना-तपश्चर्या के दबाव से संचित कुसंस्कारों को गलाने और उन्हें सुसंस्कारिता के ढांचे में ढालने का क्रियात्मक उपाय। चिन्तन की परिष्कृति ही योग है और चरित्र में निखार लाने वाली प्रक्रिया ‘तप’। कल्प साधना में इन दोनों का समन्वय है। प्रगति पथ पर अग्रगमन इन दो पहियों पर ही सम्भव हो पाता है। प्रश्न यह उठता है कल्प साधना के इस दर्शन को व्यवहार में किस प्रकार उतारें? दैनिक जीवन में तप तथा योग का समावेश न्यूनाधिक रूप में किस प्रकार बन पड़े? इसके लिए आहार से अन्तःकरण पर प्रभाव तथा उसके माध्यम से आंतरिक परिशोधन की प्रक्रिया को समझना होगा।
मन शरीर का एक भाग है। उसे ग्यारहवीं इन्द्रिय भी कहा जाता है। शरीर आहार से ही बनता है। इस कारण प्रकारान्तर से आहार के स्तर को ही शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का आधारभूत कारण माना गया है। अभक्ष्य को उदरस्थ करने वाला, अनावश्यक मात्रा में खाने वाला धर्मोपदेशक भले ही बन सके, साधक धर्मात्मा नहीं बन सकता। इसलिए पूजा उपचार की तरह ही कल्प-प्रक्रिया में आहार साधना पर अत्यधिक ध्यान देना होता है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा-कीर्तन एवं धर्मानुष्ठानों की तरह ही आहार में सात्विकता एवं सदाशयता का समावेश भी आत्मिक प्रगति के अनिवार्य आधारों में सम्मिलित रखा गया है। कल्पकाल की साधना को आत्मोत्कर्ष के प्रयासों में मूर्धन्य इसलिए भी कहा गया है कि इसमें धर्मानुष्ठानों से अधिक आहार नियमन पर ध्यान दिया गया है। आहार निग्रह के उपरान्त मनोनिग्रह कठिन नहीं रह जाता। मन को यदि सदाशयता की ओर मोड़ा जा सके तो दृष्टि बदलते ही आत्मिक प्रगति के मार्ग में फिर कोई बड़ी बाधा शेष नहीं बच रहती। आहार कल्प की महत्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।
आध्यात्मिक कल्प की यह प्रक्रिया वस्तुतः एक प्रकार का तप है। तप में तितिक्षा का समावेश रहता है। गीता के अनुसार ‘‘विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिनः’’ (2।59)—‘‘उपवास करने से विषय विकारों की निवृत्ति होती है।’’ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साधकों को अनुभवी, तत्वदर्शी, सदाचारी, आहार नियमन का परामर्श देते चले आये हैं। एक ही आहार का सेवन, किसी भी प्रकार के सम्मिश्रण से बचाव तथा जहां तक सम्भव हो आधा पेट ही आहार लेना—एक प्रकार का उपवास है, तप है। इसे मृदु चान्द्रायण का ही एक परिवर्धित स्वरूप समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में प्रायश्चित भी जुड़ जाने से अनुशासन-अनुबन्ध और भी कठिन हो जाता है। पूर्व में मनोभूमि प्रबल होने से और भी कड़ी तपश्चर्या साधक कर पाते थे, पर उस कृच्छ कड़े चांद्रायण की स्थिति तक न लौट कर युग धर्म के अनुरूप कल्प साधना में सरलता उत्पन्न करना ही श्रेष्ठ माना जायेगा।
उपवास की चान्द्रायण प्रक्रिया अति कठोर है। इसे लगभग एक महीने का अनुष्ठान कहना चाहिए। एक समय निर्धारित ग्रास के अतिरिक्त किसी और समय खाने का नियम नहीं है। पूर्णिमा को पन्द्रह ग्रास खाने और एक-एक घटाने का ही नियम है। अमावस्या से एक-एक ग्रास बढ़ाते चलकर पूर्णिमा को पूर्ण आहार की स्थिति में पहुंचते हैं। इस प्रकार लगभग बीस दिन ऐसी स्थिति रहती है, जिसे न खाने के बराबर ही समझना चाहिए। उस स्थिति में जिसमें कम-अधिक किया जाता है, मन को अत्यधिक कड़ी तपश्चर्या की अवधि से गुजरना होता है। इसको कठोर तो नहीं पर घर के नियमित अभ्यास से कुछ अलग-एक ही अन्न, एक ही शाक अथवा मात्र अमृताशन पर आधे पेट रहना, नित्य लगभग अस्वाद-उपवास की स्थिति में रहना भी एक प्रकार का तप है। कठोर तप जैसा चान्द्रायण में किया जाता है, करने वाले तो विरले मिलेंगे। एक दो दिन भोजन मिलना तो दूर चाय जैसी वस्तु न उपलब्ध होने पर ही पैर कांपना, सिर घूमना और नींद न आना जैसी शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर में इतनी चर्बी किसी-किसी के ही होती है जो लम्बे समय तक एक प्रकार से सर्वथा निराहार स्तर का कठोर उपवास कर सके। साथ में जिस मानसिक संतुलन की आशा अपेक्षा होती है वह तो कहीं दीख ही नहीं पड़ता। उसके अभाव में आहार साधना तो दूर-सामान्य उपासना क्रम भी सम्भव नहीं हो पाता। मन भूख के कारण बेचैन हो तो एकाग्रता, स्थिरता की स्थिति कैसे रहेगी? न रही तो भूखे रहना भले ही निभता रहे, वे अध्यात्म उपचार कैसे सधेंगे जिन्हें अपनाना कल्प साधना का मूलभूत उद्देश्य है। तपश्चर्या में उपासना भी एक अंग तो है, पर उतने भर से ही आत्म परिष्कार का समग्र उद्देश्य कहां पूरा होता है।
कल्प सूत्रों में आज के मानव की सभी दुर्बलताओं, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर जो संतुलित आहार साधना क्रम बनाया गया है, उसका बड़ा स्वरूप तो यह है कि साधक मात्र एक समय आधा पेट भोजन से काम चलायें। यह आहार भी एक ही अन्न हो, भांति-भांति के सम्मिश्रण न हों। इसे दो बार में बांटना हो तो मृदु स्वरूप में कुल आहार को सुबह तथा शाम दो बार में बांट सकते हैं। कहने का आशय यह है कि कुल मिलाकर आधा भोजन किया जाय एवं एक ही प्रकार के आहार द्वारा अधिक से अधिक मनःसंतुलन का अभ्यास किया जाय।
आमतौर से लोग दो समय भोजन करते हैं। इसलिए यह मान लिया गया है कि एक समय भोजन करने से काम चलाया जाना चाहिए। यह आहार उतना ही होना चाहिए जितना कि नित्य प्रति होता है। शाम के बदले का भी दोपहर को खाने की, इसी समय दूना, ड्यौढ़ा कर लेने की चतुरता करनी हो तो बात दूसरी है।
ऊंट एक दिन पानी पीकर एक सप्ताह तक रेगिस्तान में चल लेता है। उतना पानी पेट में भर लेता है कि एक सप्ताह तक फिर पीने की आवश्यकता न पड़े। मगर भेड़ के बच्चे को, सांप-मेढ़क को, व्याघ्र-हिरन को इतनी मात्रा में खा लेता है कि फिर कई दिन तक मुख खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीर्थ-पुरोहित भी ऐसा ही करते हैं। एक समय में इतना ‘छक’ लेते हैं कि दूसरे समय की तो बात ही क्या-दूसरे दिन भी न मिले तो पेट कुछ मांगेगा नहीं। यह नीति कल्प साधकों को अपनानी हो तो फिर उपवास वैसा ही मखौल बन जायेगा जैसा कि एकादशी व्रत करने वाले तथाकथित फलाहारी माल-मलाई इतनी ठूंस लेते हैं कि पेट को हाहाकार करना पड़े। साधकगण भी ऐसी ही दिल्लगीबाजी उपवास में करने लगे तो यह तपश्चर्या न रहकर आत्म-प्रवंचना ही बन जायेगी।
गायत्री तीर्थ की उपवास चर्या को ऐसा संतुलित रखा गया है कि उससे न खाली पेट रहने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई का सामना करना पड़े और न पेट को विश्राम मिलने के उद्देश्य में व्यतिरेक उत्पन्न हो। मात्रा घटाना तो हर हालत में आवश्यक ही है। दोपहर को उतनी ही मात्रा में निर्धारित आहार लिया जाय, जितना कि आमतौर से लिया जाता है। न कम, न अधिक। इसी में कल्प काल की तप-तितिक्षा की सार्थकता भी है।
इस साधना के साथ अस्वाद व्रत भी जुड़ा है। बिना मसाले का, नमक का भोजन खाने का सबका अभ्यास भी नहीं होता। प्रकृति में विद्यमान लौकी, तोरई, गाजर, परवल जैसे शाक, खरबूजा, आम, पपीता जैसे सस्ते फलों पर ही निर्वाह भी एक माह तक किया जा सके तो मानना चाहिए कि एक बहुत बड़ी तप साधना आज के युग में सध गयी। शाकाहार व दुग्ध आहार कल्प से भी सीधी सादी अमृताशन अथवा एक ही आहार कल्प की साधना है। शांतिकुंज में अब ब्वाइलर व्यवस्था द्वारा भाप से अन्न, शाक या खिचड़ी को पकाकर हर साधक को वन्दनीय माताजी द्वारा अपने हाथ से दिया जाता है। अपनी खुराक को निर्धारित करने का आत्मानुशासन साधक को अपनाना होता है। पकने के पूर्व वन्दनीय माताजी अपने हाथ से संस्कारित जल तथा औषधि, सही मात्रा में हल्दी प्रत्येक के पात्र में डालती हैं। पकने पर सभी साधक अपने-अपने पात्र अपनी कोठरी में ले जाकर ग्रहण करते हैं व उसी में संतोष करते हैं। पदार्थ की कारण-शक्ति के माध्यम से अन्तः की चिकित्सा का यह निर्धारित विधान सभी को रुचता भी है। साथ में जड़ी-बूटी का कल्प भी जुड़ जाने से समग्र कायाकल्प की संभावनाएं सुनिश्चित बन जाती हैं। आहार कल्प एवं जड़ी बूटी कल्प के व्यवहार पक्ष को अलग से समझाया गया है। यहां तो मात्र उसका दर्शन एवं कायाकल्प की सुनिश्चितता का स्पष्टीकरण है। हर साधक को अध्यात्म उपचारों को उत्तरार्ध तथा आहार साधना को कल्प का पूर्वार्ध मानना चाहिए।
वैसे कल्प में दुग्ध, मट्ठा अथवा फलाहार किसी भी एक की पूरी छूट है। लेकिन फलाहार की तुलना में शाकाहार कहीं अधिक सस्ता एवं लाभदायक बैठता है। माता का संतुलन भी ऐसा बंट जाता है कि कुसंस्कारी पाचन संस्थान को नये ढर्रे में ढलने में कोई कठिनाई नहीं होती, ‘कल्क’ कच्छा बन जाने से नित्य पेट का शोधन होता रहता है तथा उदरशूल, कब्ज, अपच जैसी कठिनाई भी नहीं रहती। वैसे गेहूं का दलिया अथवा अमृताशन भी एक प्रकार से शाकाहार या फलाहार के समतुल्य ही है। जिसका मनोबल हो वे एक महीने शाकाहार या अमृताशन पर निभा सकते हैं। उनके लिए स्वयं पका लेने के सभी साधन शांतिकुंज में मौजूद हैं। जो खिचड़ी, दाल, चावल, दलिया आदि स्वयं पका सकें, उनके लिए वैसी सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाती है। शांतिकुंज के भोजनालय में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। शाक, कोयला, अंगीठी, बर्तन, दलिया, चावल, दाल आदि सभी वस्तुएं हर किसी के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें जैसी सुविधा हो वे वैसी व्यवस्था कर सकते हैं।
आहार की मात्रा पर इतना अंकुश रखा गया है जिससे पेट सर्वथा खाली भी न रहे और उपवास की मर्यादा के अन्तर्गत उसे सीमित मात्रा में खाली भी रखा जा सके। अमृताशन उस आहार को कहते हैं जिसे भगौने में पकाया जा सके। चावल, दाल, दलिया, दूध, खिचड़ी, शाकाहार जैसे उबालकर बनाये जाने वाले सभी पदार्थ अमृताशन की मर्यादा में आते हैं। उन्हें उपवास में सम्मिलित किया जाय और फलाहार समतुल्य माना जाय तो हर्ज नहीं।
आहार पर चढ़े हुए कुसंस्कारों का परिशोधन करने के लिए गौ मूत्र की महत्ता शास्त्रकारों ने बताई है। इन दिनों जिस प्रकार खाद्य पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं उससे उनकी सात्विकता चली जाती है और ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिन्हें तामसिक ही कहा जा सकता है। रासायनिक खादों का, सीवर लाइनों की गन्दगी का उपयोग अधिक उपज लेने की दृष्टि से किया जाता है। कीड़े मारने की दवाएं फल पर व गोदामों में छिड़की जाती हैं। फिर उनके बोने, उगाने वालों के भी अपने संस्कार होते हैं जो खाद्य पदार्थों में मिले होते हैं। फलतः उन पर अदृश्य कुसंस्कारिता छाई रहती है। अध्यात्मवादी का आहार कुसंस्कारिता से रहित होना चाहिए। ‘‘जैसा खाये अन्न वैसा बने मन’’ के प्रतिपादन में साधक की साधना का प्रथम चरण सात्विकता से आरम्भ होता है। सात्विकता का अर्थ सुपाच्य ही नहीं सुसंस्कारी भी है। पकाने-परोसने में भी इस सुसंस्कारिता का समावेश होना चाहिए। वैसी सुविधा न हो तो फिर अपने हाथ ही पकाना उत्तम है। साधक स्वपाकी रहे तो दूसरे के द्वारा पकाए आहार की तुलना में इन दिनों इस सन्दर्भ में अधिक निश्चिंतता रह सकती हैं।
खाद्य पदार्थों को गौ मूत्र से परिशोधन की प्रक्रिया चान्द्रायण की भोजन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। जौ, तिल, चावल आदि खाद्य पदार्थ गौ मूत्र में भिगोकर बोने, उगाने, जमा करने की अवधि में चढ़े हुए कुसंस्कारों से मुक्त किया जाता है। सफाई करने से लेकर आटा पीसने, दाल दलाने की आश्रम में निजी व्यवस्था है। बाजार की तुलना में कहीं अधिक महंगी पड़ती है फिर भी प्रबन्ध यही किया गया है कि भले ही अन्नाहार हो पर उस पर सुसंस्कारिता फलाहार से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी हो। चान्द्रायण साधना में गौ सान्निध्य का अत्यधिक माहात्म्य बताया जाता है। गौ मूत्र सेवन की भी चर्चा है। इसका प्रतीक रूप में परिपालन कल्प साधना में किया जाता है। पंच गव्य में गौ दुग्ध, गौ दधि, गौ घृत की प्रमुखता रहती है। गौमूत्र की कुछ बूंदें ही सही पर प्रायश्चित परम्परा के अनुसार समावेश उसका भी आंशिक रूप से रहता है। इसके अतिरिक्त जो भी धान्य साधक इस एक महीने की अवधि में सेवन करते है वह सभी गौ मूत्र में भिगोया-भिगोकर गंगाजल से धोया-धोकर सुखाया और सुखाकर आश्रम में ही पीसा गया होता है। बनाने की प्रक्रिया दो ही हैं या तो माताजी के चौके में बना हो या अपने हाथों पकाया गया हो। बाजारू वस्तुएं खाने, खरीदने पर पूरी रोक हो। चटोरेपन से लालायित होकर बाजारू चीजें खरीदना-खाना पुरानी आदत को भले ही रुचिकर लगे पर उससे तपश्चर्या की व्यवस्था बिगड़ती है। अपने कक्ष में आहार को करते समय भी यह संयम बनाये रखना अत्यन्त अनिवार्य है।
उपवास पक्ष पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पेट को खाली रखना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। उसका मूलभूत प्रयोजन सात्विक, सुसंस्कारी, चटोरेपन से रहित आहार अपनाना भी है। पेट पर वजन कितना लदा, कितना हल्कापन रखा गया इस सम्बन्ध में थोड़ी रियायत समय की स्थिति को देखते हुए दी गई है। परिस्थितियों की विवशता, लोगों की स्वल्प तितिक्षा क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही यह शिशु या चान्द्रायण जैसा उपक्रम अपनाया गया है। इतने पर भी इस आध्यात्मिक प्रयोजन के निमित्त की गई आहार चिकित्सा में सैद्धांतिक कड़ाई यथावत् कायम रखी गई है। आहार की सात्विकता, सुसंस्कारिता, औषधि स्तर की स्थिति हर हालत में कायम रखी ही जानी चाहिए। चटोरेपन की अभ्यस्त आदत तथा पेट को ठूंस-ठूंस कर गधे की तरह लादे रहने की विद्रूपता तो हर हालत में रोकी या छोड़ी जानी है। इतनी व्रतशीलता अपना लेने पर कल्प साधना की उपवास प्रक्रिया अक्षुण्ण रखी जा सकेगी। भले ही आहार की मात्रा के सम्बन्ध में कुछ शिथिलता सुविधा जुड़ी रहे।
आयुर्वेदीय कल्प चिकित्सा में कई फल शाकों के कल्प का उल्लेख है। खरबूजा, आम, जामुन, पपीता जैसे सस्ते फलों पर 40 दिन रहकर यह कल्प होते हैं। महंगे फलों में अनार, मौसमी आदि के रसों पर भी रहा जाता है। सेव, चीकू भी ऐसे ही उपयोगी फलों में हैं। शाकों में टमाटर, तोरई, लौकी भी उस प्रयोजन के लिए उपयोगी होती है। दूध, छाछ के कल्पों का भी विधान है। कल्प काल में कई औषधियां भी सेवन कराई जाती हैं। पर आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए कल्पों में एक महीने की अवधि उपरोक्त फलों, शाकों में से किसी एक का चयन करके उसी पर निर्वाह किया जाय तो इससे शरीर शोधन एवं मानसिक भावनात्मक परिष्कार का भी अतिरिक्त लाभ मिलता है।
तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, गिलोय, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों का भी कल्प कराया जाता है। उनका रस, क्वाथ-कल्प या अर्क बनाकर पिलाने की प्रक्रिया है। किस-किस औषधि का कल्प कराया जाय, किस रूप में किस मात्रा में उसे दिया जाय यह निर्धारण व्यक्ति विशेष की स्थिति को समझकर उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जा सकता है।
साधारणतया इस रूप में उपरोक्त औषधियों को एक दिन में सौ ग्राम तक दिया जाता है। अर्क पिलाना हो तो उस रूप में लगभग दस औंस तक औषधियों का सार तत्व पेट में पहुंचाया जा सकता है। औषधि कल्प में फलाहार ऐसा चुना जाता है जो इन औषधियों का सजातीय है। कल्प साधना में मनोबल सम्पन्न साधकों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार इस प्रकार के अतिरिक्त कल्पों का भी निर्धारण किया जाता है।
कल्प अवधि में साधक नित्य गंगाजी जाते हैं। अपने पीने के लिए गंगाजल का पात्र स्वयं भरकर लाते हैं। जब भी पीना हो तो उसी को पीते हैं। इस प्रकार गंगा और गौ का सान्निध्य रहने के अतिरिक्त एक अध्याय गीता एवं प्रज्ञापुराण का सामूहिक पाठ भी होता है। गायत्री के 24 हजार अनुष्ठानों अथवा सवालाख अनुष्ठान का सम्पुट तो साथ-साथ है ही। इस प्रकार गंगा, गौ, गीता और गायत्री के रूप में प्रख्यात अध्यात्म साधना के चारों चरणों को अपनाते रहकर साधक अपनी पवित्रता, प्रखरता एवं प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। कायाकल्प के विषय में पहले ही कहा जा चुका है कि यह मात्र पुराने अभ्यासों के ढर्रे को बदलकर नवीन जीवनक्रम आरम्भ करना है। शरीर शोधन तो अवश्य होता है पर अन्तः में कायाकल्प व शारीरिक बलिष्ठता में बड़ा अन्तर है। अपना भावी जीवन कष्ट साध्य न हो, निरोग, दीर्घायुष्य काया का आनंद प्राप्त हो, साथ ही आत्मिक प्रगति का प्रयोजन सधा रहे उसी का यह पूर्वाभ्यास है। आहार से श्रेष्ठ और कोई माध्यम इसके लिए नहीं हो सकता। च्यवन, ययाति की तरह यौवन प्राप्ति पुनः हो सकी कि नहीं, इसे नहीं बल्कि जीवनी शक्ति सम्वर्धन एवं नवीन जीवन पद्धति के अभ्यास की दिशाधारा मिल जाने को ही एक माह की साधना का अनुदान, वरदान मानना चाहिए। चिन्तन, शरीर क्रिया, व्यवहार तथा अन्तः का परिपूर्ण काया कल्प ही वास्तविक कल्प साधना है। अनगढ़ शरीर व मन इस एक माह में प्राकृतिक जीवन क्रम को आगे भी अपनाने के लिए विवश हो जाय, यही इस आहार साधना का मुख्य उद्देश्य है।
Write Your Comments Here:
- अध्यात्म क्षेत्र की उच्चस्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग
- कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
- साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलम्बन
- आन्तरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता
- कर्मफल की सुनिश्चतता : एक महत्वपूर्ण तथ्य
- दुष्कृतों के अवरोधों को हटाने की साहसिकता उभरे
- पापों का प्रतिफल और प्रायश्चित-शास्त्र अभिमत
- समस्त व्याधियों का निराकरण— आध्यात्म उपचार से
- प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
- हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
- क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
- कल्पकाल की आहार साधना
- आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
- अन्तर्मुखी प्रवृत्ति और निरन्तर आत्म-दर्शन
- जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
- आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन
- कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं
- कल्पकाल की अति फलदायी ऐच्छिक साधनायें
- आहार एवं औषधिकल्प के मूल सिद्धांत एवं व्यावहारिक स्वरूप
- आहार सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियां एवं उनका निवारण
- कल्प के पूर्व कुछ अनिवार्य ज्ञातव्य
- कल्प चिकित्सा की पात्रता के सम्बन्ध में महर्षि चरक का मत
- विभिन्न प्रकार के कल्प प्रयोग
- कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार