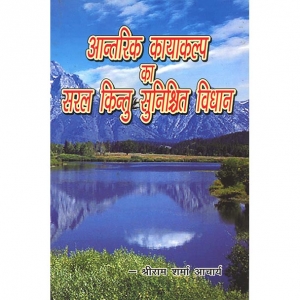आन्तरिक कायाकल्प का सरल किन्तु सुनिश्चित विधान 
आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
Read Scan Versionउपवास पूर्वक स्वालक्ष गायत्री अनुष्ठान प्रायः लोग अपने घरों पर भी करते रहते हैं। उपवास में आमतौर से आधे पेट से अधिक भोजन नहीं किया जाता। पेटू लोगों की बात अलग है जो उपवास जैसी तपश्चर्या को भी मात्र आहार परिवर्तन भर समझते हैं और पेट पर अन्य दिनों की अपेक्षा भी अधिक बोझ लादते हैं। कल्प साधना में आधे पेट भोजन का प्रबन्ध तो हो ही जाता है। ऐसी दशा में चान्द्रायण जैसा स्वरूप नहीं रह जाता जैसा कि शास्त्रकारों ने उसका असाधारण माहात्म्य वर्णन किया है। आहार चिकित्सा की बात हो तो वह भी अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की तरह लोग अपने-अपने काम धन्धे के साथ-साथ करते रह सकते हैं।
जिस विशेषता के कारण देखने में साधारण किन्तु परिणाम में महान इस तपश्चर्या का माहात्म्य बताया गया है वह है—‘आत्मिक कायाकल्प’, जिसके निमित्त इस सन्दर्भ में अनेकानेक नियम, संयम एवं विधि-विधानों का निर्धारण हुआ है। उपवास और जप तो उस प्रक्रिया के दृश्यमान शारीरिक क्रिया-प्रक्रिया के रूप में सम्पन्न होने वाले उपचार भर हैं।
वस्तुतः इस साधना को अध्यात्म कल्प उपचार समझा जाना चाहिए और उसके साथ प्रयोजनों का महत्व समझा जाना चाहिए जो उसके साथ चिन्तन और भावना के रूप में अविच्छिन्न रूप में जुड़े हुए हैं। यदि उन पर ध्यान न दिया जाय और केवल शरीरचर्या चलती रहे तो समझना चाहिए कि शास्त्र निर्धारण का एक बहुत छोटा अंश ही पूरा हुआ।
समझा जाना चाहिए कि अध्यात्म तत्वज्ञान भावना एवं विचारणा के क्षेत्र पर प्रयुक्त एवं प्रभावी होता है। वहां प्रखरता उत्पन्न हो तो शरीर के क्रिया कलाप अनायास ही उत्कृष्टता युक्त बन जाते हैं। भक्तियोग में भावना क्षेत्र को श्रद्धा तत्व से परिपूर्ण बनाया जाता है। योग प्रज्ञा की आराधना है। इन दोनों को उच्चस्तरीय भाव संवेदना एवं उदात्त दृष्टिकोण का उन्नयन अभ्युदय कहा जा सकता है। भक्तियोग, ज्ञानयोग के द्वारा अन्तःकरण एवं विचार संस्थान को अधिक परिष्कृत बनाया जा सके तो कर्मयोग अनायास ही निभने लगता है। शरीर तो वाहन उपकरण भर है। उसे अन्तःप्रेरणाओं के निर्देशन में काम करना होता है। वह स्वामिभक्त सेवक की तरह सभी भले-बुरे निर्देशनों का पालन करने में सर्वथा तत्पर रहता है।
कहने को तो कर्मयोग स्थूल शरीर का, ज्ञानयोग सूक्ष्म शरीर का, भक्तियोग कारण शरीर का विषय कहा जाता है, किन्तु थोड़ा गहराई में उतरने पर प्रतीत होता है कि विभाजन की दृष्टि से बनी हुई इस त्रिविध क्रिया-प्रक्रिया का उद्गम स्रोत एक ही है—आस्था का परिष्कार। मशीन के दांतों की तरह एक ही प्रेरणा से दूसरा घूमता है। दूसरे के दबाव से तीसरे में हलचल बन पड़ती है। आस्थाएं ऊंची हों तो विचार-संस्थान को उनका अनुगमन करना होगा, विचारों का निर्देशन शरीर मानता है। उसे अपने कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं देखा जाता। समूचे व्यक्तित्व का पवित्रीकरण-प्रखरीकरण ही अध्यात्म तत्वज्ञान एवं साधना विज्ञान का एक मात्र उद्देश्य है। उसी की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की दार्शनिक दिशा धाराओं का सृजन हुआ है।
ब्रह्मविद्या का विशाल कलेवर इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए तत्वदर्शियों ने सृजा है। इसी प्रकार साधना विधान के अन्तर्गत क्रिया-प्रक्रियाओं का उद्देश्य एक ही है—देव जीवन की दृष्टि से हेय समझी जाने वाली मान्यताओं एवं आदतों का निराकरण तथा सदाशयता को स्वभाव में सम्मिलित करने का अभ्यास। पशु प्रवृत्तियों को बदलने के लिये जो भावना और प्रक्रिया का सम्मिलित पुरुषार्थ किया जाता है, उसी को साधना कहते हैं। साधनाकाल में अपना चिंतन तथा व्यवहार ऐसा बनाना पड़ता है जिनके दबाव से व्यक्तित्व की गहन परतों में प्रविष्ट अभ्यस्त आदतों में अभीष्ट परिवर्तन सम्भव हो सके।
भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग की त्रिवेणी में अवगाहन करने से ही आत्मिक प्रगति का पथ-प्रशस्त होता है। इन तीनों के स्वप्न देखते रहने से काम नहीं चलता। अध्ययन, श्रवण के माध्यम से मिलने वाले परामर्श इस दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं किन्तु इतने भर से पुराना ढांचा-ढर्रा बदलता नहीं। वह गहरी परतों में अपनी जड़े जमाये बैठा रहता है। फलतः धर्मजीवी व्यक्ति तक हेय जीवन जीते देखे गये हैं। व्यक्तित्व के परिष्कार में साधना उपचार का दबाव पड़े बिना काम नहीं चलता। धातुओं को कोई रूप देना हो तो उसके अग्निसंस्कार की अनिवार्य आवश्यकता पड़ेगी। साधना को एक प्रकार से ढांचे का रूपान्तर कहा जा सकता है। इसके लिए साधना तपश्चर्या को आग-भट्टी के समतुल्य माना जा सकता है।
कल्प साधना में भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग की त्रिविध क्रिया-प्रक्रियाओं का समन्वय है। गायत्री उपासना एवं ध्यान-धारणा को भक्तियोग समझा जाना चाहिए। स्वाध्याय-सत्संग स्थूल और चिन्तन मनन सूक्ष्म ज्ञानयोग की पूर्ति करता है। व्रत-उपवास के अनुशासक कर्मयोग का अभ्यास कराते हैं। इस समन्वय से तीनों शरीरों को परिष्कृत करने वाली तीन प्रकार की विधि-व्यवस्था के अन्तर्गत समूचे व्यक्तित्व की ढलाई-गलाई होने लगती है। इस समग्र समन्वय की कार्यपद्धति से ही कल्पसाधना का तात्विक प्रयोजन पूर्ण होता है। मात्र उपवास या जप का उपक्रम चलता रहे और हर क्षेत्र को उत्कृष्टता की दिशा में धकेलने वाले अन्यान्य अनुबन्धों की उपेक्षा होती रहे तो समझना चाहिए कि बाह्य कलेवर की ही व्यवस्था बनाई गई है। उसमें प्राणसंचार करने वाली आध्यात्मिक प्रखरता उत्पन्न करने में समर्थ भावनात्मक तपश्चर्याओं का समावेश नहीं किया गया है। सर्वविदित है कि कलेवर कितना ही सुन्दर क्यों न हो, उसमें प्राण नहीं होगा तो अभीष्ट हलचल उत्पन्न होने और परिणति का लाभ मिलने जैसा अवसर ही उत्पन्न न होगा।
कल्प साधना के साथ जुड़े हुए उपरोक्त तथ्यों को समझने के उपरान्त ही वह सरंजाम जुटाना सम्भव हो सकेगा जिसके फलस्वरूप शास्त्रवर्णित सत्य परिणामों की सम्भावना को प्रत्यक्ष होते हुए देखा जा सकेगा। समग्र व्यवस्था का परिणाम ही समग्र होता है। आवश्यक सभी साधन जुटने पर ही महत्वपूर्ण कार्यों का सूत्र संचालन होता है। रसोई बनानी हो तो आग, बर्तन, खाद्य पदार्थ, पानी आदि सभी चीजें चाहिए। इनमें से किसी एक को पकड़ बैठा जाय तो पेट भरने का सरंजाम किस प्रकार बनेगा। बढ़ई, लुहार, दर्जी, चित्रकार, मूर्तिकार आदि को सभी उपकरण एकत्रित करने पड़ते हैं। यदि उनके हाथ में एक ही औजार हो तो कुछ कारगर निर्माण बन नहीं सकेगा। अकेली सुई लेकर दर्जी, आरी लेकर बढ़ई, हथौड़ा लेकर शिल्पी अपनी कलाकारिता का परिचय दे नहीं सकता। बात तभी बनेगी जब सभी आवश्यक उपकरण जुटाकर समग्र व्यवस्था बनाने की तैयारी चल पड़े।
कल्प में उपवास की प्रमुखता से किसी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि देवता को प्रभावित करने एवं आसमान से वरदान खींच लेने के लिए इतना सा स्वल्प उपचार अपनाने भर से काम चल जायेगा। जितना महत्व शरीर साधना के रूप में उपवास अनुष्ठान का है, उससे कम आवश्यक श्रद्धा एवं प्रज्ञा को प्रभावित करने वाली उस विधि-व्यवस्था का भी नहीं है जो अन्तःकरण को मथ डालती है, चिंतन की दिशाधारा बदलती है और स्वभाव तथा अभ्यास में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित करती है।
इस साधना को कल्प साधना कहा गया है। शरीरगत कल्पचिकित्सा की पृष्ठभूमि अनेकों को विदित है। उसी आधार पर चिंतन और चरित्र को उलट देने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जाना चाहिए।
कायाकल्प के प्रयोग जिनने देखे या सुने-समझे हैं, वे जानते हैं कि रुग्ण, दुर्बल एवं अस्त-व्यस्त काया संस्थान को नये सिरे से सुधारने सम्भालने की प्रक्रिया ‘कल्प’ कहलाती है। इसमें पुराने जीवकोशों को हटाकर नये जीव कोशों का ढांचा नये प्रकार का बन सके ऐसा प्रयत्न किया जाता है। सांप के केंचुली बदलने से इसकी उपमा दी जाती है। सांप पुरानी चमड़ी को किसी पेड़ से अटकाकर बदल देता है और जो नई निकलती है, उसका उपयोग करता है। केंचुल भारी होने पर सांप के लिए दौड़ना तो दूर चलना फिरना तक भारी हो जाता है। किन्तु जब पुराने कलेवर का परित्याग कर दिया जाता है तो उसे नई चमड़ी नई काया की तरह नई स्फूर्ति प्रदान करती है। उसकी शोभा ओर शक्ति दोनों ही बढ़ा देती है। कल्प चिकित्सा को भी इसी प्रकार के केंचुल बदलने की उपमा देकर समझाया जाता है।
स्वर्गीय महामना मालवीय जी ने अपनी कल्प चिकित्सा कराई थी। समग्र रूप से न बन पड़ने पर भी बहुत लाभकारी हुई थी। उसकी सुखद परिणति का विवरण उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया था। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आयुर्वेद शास्त्र में उस प्रक्रिया के उपलब्ध होने पर भी सामयिक परिस्थितियों में उसका उपयोग कैसे करना चाहिए इस संदर्भ में कोई ठोस प्रयास नहीं हुए। यदि उन निर्धारणों का पुनरुद्धार सम्भव हो सका होता तो निश्चय ही मनुष्य जाति की महती सेवा बन पड़ती। जरा जीर्ण ययाति की तरह नवयौवन प्राप्त करने का अवसर मिलता। कितने ही वयोवृद्ध अपनी वृद्धावस्था को नवयौवन में बदल सकते, अशक्तता हटाकर अभिनव सामर्थ्य प्राप्त कर सकने का सौभाग्य कितना सुखद एवं सौभाग्यशाली हो सकता है। आज तो उसकी कल्पना ही की जा सकती है।
महामना मालवीयजी ने कल्प कराया था तब उन्हें चालीस दिन तक एकान्त पर्णकुटी में रहना पड़ा था। इतने दिनों तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था ताकि जो परिवर्तन हो रहा है उसे बाहरी वातावरण प्रभावित न करने पाये। शौच, स्नान, भोजन आदि का सारा प्रबन्ध भीतर ही होता था। वे धूप सेवन तक के लिए बाहर नहीं निकले थे। सभी नित्यकर्म उसी बन्द पर्णकुटी में होते थे। इस अवधि में आहार, शयन, औषधि, शारीरिक हलचल के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध थे वे विधिवत् पूरे करने पड़े थे। साथ ही सोचने के लिए, कल्पना-आकांक्षा के लिए एक निश्चित सीमा बना दी गई थी कि वे न केवल शरीर को वरन् विचारों को भी उसी परिधि में अपनी दौड़ सीमित रखने के लिए विवश करें। वैसा ही किया गया था।
उपरोक्त विधान पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि ऐसे उपचारों में अभिनव निर्धारण को जीवनचर्या में पूरी तरह समाविष्ट होने का अवसर दिया जाता है। साथ ही परातन अभ्यासों को, बाहरी वातावरण के दबावों को उन दिनों न पड़ने देने की विशेष रूप से रोकथाम की जाती है। महान् परिवर्तन के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है।
भ्रूण को नौ माह तक माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अण्डे के कड़े छिलके का आच्छादन उसके भीतरी भाग को चारों ओर से घेरे रहता है। इससे दोनों प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बाहरी दबाव से बचाव भी और भीतरी क्षेत्र में समयानुसार पकने, परिपक्व होने की सुविधा भी इस आच्छादन से मिलती है। इस संरक्षण के अभाव में न तो गर्भस्थ शिशु का विकास होगा, न अण्डा पकेगा। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि उन्हें बाहरी गर्मी मिलनी चाहिए। अण्डे के ऊपर मुर्गी अपनी छाती लगाये बैठी रहती है और उसे आवश्यक गर्मी प्रदान करके पकने की स्थिति तक पहुंचाती है। पेट के बच्चे को भी माता गर्मी की, आहार की व्यवस्था अपने शरीर अनुदान द्वारा प्रदान करती है। यह भी एक प्रकार का कायाकल्प ही हुआ। अपनी इस विशिष्ट साधना को भी आत्मिक कल्पसाधना का रूप दिया गया है। उसके लिए सर्वप्रथम उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसा वातावरण जहां अनुपयुक्त वातावरण से बचाव हो सके, उपयुक्त सुविधा तथा अनुभवी मार्गदर्शन उपलब्ध हो एवं उस प्रयास को सफल बना सकने वाला सहयोग अनुदान मिल सकने की व्यवस्था हो। निश्चय ही यह व्यवस्था घर के वातावरण में रहकर सम्भव नहीं हो सकती। अभ्यस्त ढर्रा अनायास ही अपनी ओर खींचता रहता है। पुरानी आदतें तथा स्थानीय समस्याएं नये प्रयास में मन को पूरी तरह लग सकने जितना अवसर नहीं देतीं। आदतें बदलनी हों तो वातावरण भी बदलना चाहिए। चोरों को जेलखाने में इसीलिए रखा जाता है कि पुराने सम्पर्क एवं कार्यक्षेत्र से अलग रखकर उसे नयी रीति-नीति अपनाने के लिए विवश किया जा सके। जेल प्रतिशोध, उत्पीड़न के लिए नहीं, सभ्य देशों में सुधारगृह की तरह प्रयुक्त की जाती है। यही बात योगियों के वन की गुफा, कन्दराओं में रहकर स्वेच्छापूर्वक एकान्त सेवन वाली व्यवस्था में भी सन्निहित है। वे अपने को नये ढांचे में ढालना चाहते हैं किन्तु चारों ओर फैला हुआ वातावरण उन्हें अभ्यस्त शिकंजे की जकड़नों से बाहर नहीं निकलने देता। कठिनाई का हल न देखकर वे उतने समय के लिए एकान्त के निमित्त चले जाते हैं जितने में अभ्यस्त ढर्रे को बदलने की मंजिल दूर तक पार न कर ली जाय। गुरुकुल आरण्यकों की शिक्षा पद्धति में भी यही विशेषता है।
भगवान राम को तप-साधना के लिए अयोध्या छोड़कर हिमालय जाना पड़ा था। चारों भाई गुरु वशिष्ठ की गुफा के इर्द-गिर्द अपनी-अपनी पर्णकुटी बना कर रहे थे। यों अयोध्या में सुविधाजनक निवास की उनके लिए कोई कमी कठिनाई नहीं थी। फिर भी देखा गया कि उस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए चिरकालीन सम्बन्ध किसी न किसी बहाने खटपट करते रहेंगे और चित्त में विक्षेप रहने से आन्तरिक परिष्कार के लिए आवश्यक सुविधा जुटेंगी नहीं। अस्तु उन्हें लाभ के लिए छोटी हानि उठाने का सिद्धांत अपनाकर वन गमन करना पड़ा। यही परंपरा अन्य ऋषि तपस्वी अपनाते रहे हैं। उन्हें अपनी जन्मभूमि के स्थान सम्बन्धी असुविधा नहीं थी किन्तु वातावरण घर खींच कर कैसे लाया जाय? गंगा अपने घर आने के लिए किसी प्रकार सहमत की जाय ऐसा न होकर अपने को ही उसके पास जाना पड़ता है। उच्चस्तरीय साधना के लिए जैसे वातावरण की, साधन-सुविधा की आवश्यकता है उसके लिए अभी भी गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि एवं उपयुक्त मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं गायत्री तीर्थ जैसे स्थानों में उपलब्ध हो सकती हैं।
कल्प अवधि का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन दिनों का तीर्थ सेवन स्थान की दृष्टि से ही एकांत न माना जाय वरन् पूर्णतया अन्तर्मुखी रहा जाय। यह समय विशुद्ध रूप से अन्तर्जगत में प्रवेश करने का है। इसमें अन्तराल की आत्मसत्ता का अति गम्भीरतापूर्वक निरीक्षण परीक्षण किया जाय। जो अवांछनीयताएं स्वभाव का अंग बन गई हैं उनके दुष्परिणामों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय और देखा जाय कि सामान्य सी लगने वाली ये छोटी-छोटी दुष्प्रवृत्तियां कितनी विघातक होती हैं। लकड़ी में घुन, कपड़े में आग, शरीर में विष की मात्रा थोड़ी होने पर भी वे जहां बसते हैं, वहां धीरे-धीरे विनाशलीला रचते रहते हैं और अन्ततः सर्वनाश करते छोड़ते हैं। इस कुसंस्कारिता की गंदगी को हर कोने में बुहार-बुहार कर इकट्ठी करना और ऐसे स्थान पर पटकने की बात सोचना चाहिए जहां से उसकी फिर वापसी न होने पाए। कल्पसाधना के दिनों में अन्तर्मुखी होकर यह बुहारने का काम रुचिपूर्वक किया जाना चाहिए। साथ ही शेष आधा चिन्तन इस तथ्य पर नियोजित रखना चाहिए कि जिन सत्प्रवृत्तियों का संचय सम्वर्धन अभी तक नहीं किया जा सका उनकी पूर्ति के लिए दूरगामी योजना बना ली जाय और उसका शुभारम्भ इन्हीं दिनों में व्रतशील होकर कर दिया जाय।
आत्म निरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्मविकास के चार चरण आत्मिक प्रगति के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। मनः संस्थान एवं भाव संस्थान को इन दिनों पूरी तरह उसी क्षेत्र को सुव्यवस्थित एवं उज्ज्वल सम्भावनाओं से भरा पूरा बनाने में निरत रखा जाना चाहिए। उपवास, अनुष्ठान एवं आहार कल्प तो साथ-साथ चलता ही रहेगा।
Write Your Comments Here:
- अध्यात्म क्षेत्र की उच्चस्तरीय सफलताओं का सुनिश्चित राजमार्ग
- कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप
- साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलम्बन
- आन्तरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता
- कर्मफल की सुनिश्चतता : एक महत्वपूर्ण तथ्य
- दुष्कृतों के अवरोधों को हटाने की साहसिकता उभरे
- पापों का प्रतिफल और प्रायश्चित-शास्त्र अभिमत
- समस्त व्याधियों का निराकरण— आध्यात्म उपचार से
- प्रायश्चित का पूर्वार्द्ध—पश्चात्ताप
- हठीले कुसंस्कारों से मुक्ति प्रायश्चित प्रक्रिया से ही सम्भव
- क्षतिपूर्ति—पूर्णाहुति
- कल्पकाल की आहार साधना
- आन्तरिक परिष्कार का स्वर्ण-सुयोग
- अन्तर्मुखी प्रवृत्ति और निरन्तर आत्म-दर्शन
- जीवन-साधना में संयमशीलता का समावेश
- आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्वदर्शन
- कल्पकाल की त्रिविध अनिवार्य साधनाएं
- कल्पकाल की अति फलदायी ऐच्छिक साधनायें
- आहार एवं औषधिकल्प के मूल सिद्धांत एवं व्यावहारिक स्वरूप
- आहार सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियां एवं उनका निवारण
- कल्प के पूर्व कुछ अनिवार्य ज्ञातव्य
- कल्प चिकित्सा की पात्रता के सम्बन्ध में महर्षि चरक का मत
- विभिन्न प्रकार के कल्प प्रयोग
- कल्प उपचार का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार