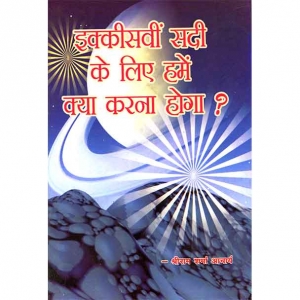ईक्कीसवी सदी के लिए हमें क्या करना होगा ? 
प्रगति के त्रिविध अवलम्बन
Read Scan Version
यह सुनिश्चित तथ्य है कि मनःस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मान्यताएं और भावनाएं ही व्यक्तित्व का गठन करती हैं। विचार बीज और कार्य उसके द्वारा उत्पादित पौधे हैं। व्यक्ति का नीतिवान, समाजनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, धर्मात्मा एवं परमार्थी बन सकना तभी संभव है, जब उसके अन्तःकरण में उत्कृष्ट आदर्शवादिता ने गहरी जड़ जमा ली हों। भ्रष्ट-चिन्तन तो दुष्ट आचरणों को ही जन्म देगा और उस विष वृद्धि के समर्थ होने पर परिस्थितियां अनर्थकारी स्तर की ही बन कर रहेंगी।
इन दिनों विज्ञान और बुद्धिवाद की अभिवृद्धि ने सुविधा-साधनों के अम्बार खड़े कर दिये हैं। पूर्वजों की तुलना में भौतिक दृष्टि से हम कहीं सुविधासम्पन्न हैं। सम्पदा की उपलब्धि को यदि प्रगति कहा जाय, तो मानना पड़ेगा कि पूर्वजों की तुलना में हम कहीं आगे हैं; पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। जनसाधारण का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह गड़बड़ा रहा है। दुर्बलता और रुग्णता दिन-दिन तूफानी गति से बढ़ती जा रही है। अस्पताल, डॉक्टर और औषधि आविष्कारों ने हमें स्वस्थ और समर्थ बनाने में कोई सहायता नहीं की है, कारण कि आहार-विहार में बढ़ा हुआ असंयम, स्वस्थ जीवन के मूलभूत आधार को ही नष्ट किये दे रहा है। पैसा बढ़ा है; पर उसके साथ ही दुर्व्यसनों और प्रदर्शनों के निमित्त होने वाले अपव्यय की इतनी वृद्धि हुई है कि हर कोई अपने को अभावग्रस्त अनुभव करता है। कामचोरी, हरामखोरी को प्रश्रय मिलते रहने पर किसी भी क्षेत्र में वास्तविक एवं अभीष्ट प्रगति हो नहीं सकती। गुण, कर्म, स्वभाव में घुसे हुए दुर्गुण आये दिन ऐसे संकट खड़े करते रहेंगे, जिनका समाधान करने में भौतिक उपचार एवं अनुदान कुछ काम न आ सकें। बढ़ते हुए अविश्वास, असहयोग, अनाचार के पीछे चरित्र-भ्रष्टता ही मूल कारण है। क्रोध से क्रोध और अनाचार से अनाचार बढ़ता है। यह विपन्नता आज संसार के समूचे जलाशय पर जलकुम्भी-काई की तरह छायी दीखती है और जलाशय से मिलने वाले लाभों का अन्त हो रहा है। पथभ्रष्ट को किस प्रकार कंटीली झाड़ियों से संत्रस्त होना पड़ता है, इसे हममें से प्रत्येक को सर्वत्र घटित होते देखा जा सकता है।
प्रदूषण, विकिरण, पर्यावरण, अपराध, छल आदि के जो संकट व्यापक रूप से घहरा रहे हैं, उनकी परिणति की कल्पना और चिन्ताजनक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक साधन जुटा सकना कठिन प्रतीत होता है। अवांछनीयता और वातावरण में संव्याप्त विपन्नता कैसे पनपी? इसका उत्तर वस्तुओं की कमी होने की बात कहने से नहीं मिल सकता। मानना यही पड़ेगा कि विचार क्षेत्र में बढ़ती हुई उद्दण्डता का, आपाधापी का प्रदूषण ही उन समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, जो अप्रसन्नता और अव्यवस्था का निमित्त कारण बनी हुई हैं।
संक्षेप में यही निष्कर्ष निकलता है कि नीतिनिष्ठा और समाजनिष्ठा के आदर्शों की अवहेलना करने पर ही समूचा मनुष्य समुदाय उस विपत्ति में फंसा है, जिससे निकलना और उबरना असंभव नहीं, तो कम से कम सहज तो प्रतीत नहीं होता है। आशा की किरण एक ही है—लोकमानस का परिष्कार, आदर्शों का परिपालन, विचारों का परिशोधन, चरित्र और प्रयासों में आदर्शों का सम्पुट लगाया जाना। उनके बिना प्रस्तुत असंख्यों समस्याओं में से एक का भी सीधा समाधान मिलना नहीं है।
उक्त महान प्रयोजन की पूर्ति अध्यात्म तत्त्वज्ञान से होती है। भावनाओं और मान्यताओं का उदात्तीकरण इसी आधार पर संभव है। प्रस्तुत विश्व-समस्याओं का निराकरण भी यही है। व्यक्तियों को भ्रान्तियों एवं अवांछनीयताओं से मुक्त करके ही उन्हें मौज से रहने और रहने देने की स्थिति में लाया जा सकता है। हंसती-हंसाती जिन्दगी, मिल-बांटकर खाने की प्रवृत्ति, झपटने-हड़पने की अपेक्षा सेवा-सहायता में रुचि लेने की रीति-नीति ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बना सकती है और उन सारी विपत्तियों से एकबारगी छुटकारा दिला सकती है, जिनके कारण कि महाविनाश की आशंका पनप रही है।
उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्रचलित भाषा में जिसे ‘‘विचार क्रान्ति’’ कहा जाता है और पुरातन सोच के अनुसार जनमानस का परिष्कार कहा जा सकता है। इस मर्यादा को अन्तःकरण की गहराई तक पहुंचाने में मात्र अध्यात्म तत्त्वदर्शन ही समर्थ हो सकता है। इस प्रकार समर्थ एवं प्रखर अध्यात्म से ही यह आशा की जा सकती है कि व्यक्ति और समाज के सामने प्रस्तुत असंख्यों विपन्नताओं-विभीषिकाओं का समाधान हो सकेगा।
इसके अतिरिक्त वह शक्ति भी जीवन्त अध्यात्म में ही है, जो सर्वतोमुखी समर्थता और प्रगतिशीलता से जनसाधारण को लाभान्वित कर सके। अध्यात्म की चर्चा सिद्धियों के संबंध में भी होती रहती है और कहा जाता रहा है कि सतयुग की वापसी जैसा सुखद वातावरण यदि उससे विनिर्मित करना हो, तो मनुष्य को समझना और समझाना पड़ेगा कि जिस प्रकार शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल, कौशल बल आदि के सम्पादन का प्रयत्न किया जाता रहा है, उससे बढ़कर आत्म बल का उपार्जन-अभिवर्धन होना चाहिए। उज्ज्वल भविष्य की संरचना इसी आधार पर हो सकेगी। इक्कीसवीं सदी में जिन सुखद भवितव्यताओं की अपेक्षा की जा रही है, उसके लिए दैवी शक्ति के रूप में अध्यात्म का सर्वतोमुखी संवर्धन होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता एवं दूरदर्शिता यही है।
कठिनाई यह है कि परिस्थितियों को देखते हुए अध्यात्म के संबंध में इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो चली है। भौतिक विज्ञान और प्रच्छन्न अध्यात्म ने मिल-जुलकर ऐसा वातावरण बनाया है, जिससे श्रद्धा डगमगाती है और आत्म-साधना का कोई जल्दबाजी भरा परिणाम न आने से उस ओर सर्वसाधारण की प्रवृत्ति को मोड़ना अतिशय कठिन हो रहा है।
वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच बने रहस्य उद्घाटित करने के लिए दैवी-नियोजन ने सर्वसाधारण के सामने एक सुयोग प्रस्तुत किया है। शान्तिकुंज की भूतकालीन गतिविधियों में यदि कुछ आनंददायक और उत्साहवर्द्धक है, तो उसका श्रेय आत्म-शक्ति को ही जाता है। भले ही प्रयोक्ता कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो। भूतकाल में सभी का उल्लेख हो चुका। इन दिनों जो तैयारी चल रही है, उसे भी इसी स्तर का समझा जा सकता है कि कोई सर्वशक्तिमान नियोजन कार्यान्वित होने जा रहा है। उसे भी इस भाषा में कहा जा सकता है, मानों कोई सत्ता असंभव को संभव करने जा रही हो।
युग परिवर्तन के भूतकालीन, आज के और भावी प्रयत्नों को जोड़कर देखा जाय, तो इसे ‘‘आत्म शक्ति से समाज संरचना’’ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इतने पर भी पूर्व असमंजस जहां का तहां अड़ा रह जाता है कि बात यदि ऐसी है, तो इतने बड़े समुदाय द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया अपने द्वारा किसी महत्त्वपूर्ण संरचना का परिचय क्यों नहीं दे रही है?
यह साधारण असमंजस नहीं है। इसके निराकरण के ऐसे समाधानकारक प्रमाण चाहिए, जो अविश्वास को विश्वास में बदल सकें। साथ ही यह रहस्योद्घाटन भी कर सकें कि सशक्त और सही अध्यात्म का स्वरूप क्या हो सकता है, जो अपनी प्रखरता का परिचय दे सके; और साथ ही इस तथ्य से भी सर्वसाधारण को अवगत कराया जाना चाहिए कि वे अभाव क्या हैं, जिनकी उपेक्षा के कारण पूजा-पत्री और कथा-वार्ता मात्र विडम्बना बनकर रह गयीं। दिग्भ्रान्त लोगों को इसी कारण से ऐसी असफलताएं हस्तगत हुईं, जो न केवल उसको असमर्थ और उपहासास्पद बनाती रहीं, वरन् लोक श्रद्धा भी डगमगाती रही, विचारशीलों को उस उत्साह से वंचित भी करती रही, जिससे कि वे सही दिशाधारा अपनाकर अपने को और अपने समूचे समूह को कृत-कृत्य बनाते।
इन समस्त समाधानों के लिए शान्तिकुंज के संचालक द्वारा निजी जीवन में अपनाये गये उन तथ्यों पर प्रकाश डालना पड़ रहा है, जिसमें वे भूतकाल को साक्षी रूप में प्रस्तुत करते हुए, वर्तमान क्रिया-कलापों के औचित्य पर विश्वास करने की मनःस्थिति पैदा कर सकते हैं। साथ ही भावी योजना के लिए जितनी जनशक्ति और साधनशक्ति की अपेक्षा होगी, उसे सफल-सम्पन्न कर सकते हैं। इससे शक्ति-संचय हेतु किये गये पुरुषार्थ और तदनुरूप दैवी अनुकम्पा के सहयोग की सम्भावना का रहस्य आसानी से समझा जा सकता है।
प्रस्तोता ने पूजा-अर्चा की उपेक्षा की हो, सो बात नहीं। इस दिशा में सघन विश्वासी जो कर सकता है, वह भी उनने दुस्साहस स्तर पर पूरा किया है। पर साधना को ही उन प्रयोगों में भी अपनाया है, जिन्हें अध्यात्म का प्राण कहा जा सकता है।
कपड़े को धोने के बाद ही उस पर रंग चढ़ता है। लोहा तो भट्टी में गलने के उपरान्त ही उससे अभीष्ट स्तर के उपकरण ढलने योग्य बन पाता है। पात्रता के अनुरूप ही अनुदान मिलते हैं। इन उदाहरणों की चर्चा इस संदर्भ में की जा रही है कि अध्यात्मवादी को निजी व्यक्तित्व के परिष्कार को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसकी शोभा-सज्जा के लिए जप-तप को प्रश्रय देना चाहिए। यही है प्रयोक्ता का अनुभव और प्रतिदान, जो साक्षी रूप में इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिसने इस दिशा में चलने का साहस जुटा लिया है, उसे यह भी जानना चाहिए कि समग्र साधना-सम्पादन के लिए किन तथ्यों को अविस्मरणीय मानते हुए अपनाने की तैयारी करनी चाहिए।
इन पंक्तियों के लेखक ने अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों की प्रेरणा, अनुसंधान, अनुभव के आधार पर यह जाना और माना है कि आत्म विज्ञान की त्रिवेणी संगम की तरह तीन दिशा धाराएं हैं:— (1) उपासना (2) साधना (3) आराधना। तीनों के समन्वय से ही एक पूरी बात बनती है।
मनुष्य अन्न, पानी और हवा के आधार पर जीता है। तीन लोक प्रसिद्ध हैं। तीन देवता प्रमुख कहे गये हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य समय के तीन काल माने जाते हैं। जीव, ईश्वर और प्रकृति के समन्वय से संसार चल रहा है। इसी प्रकार यह भी माना जाना चाहिए कि (1) उपासना (2) साधना (3) आराधना का समन्वय ही आत्मशक्ति के उपार्जन को सुनिश्चित करता है। इन्हें समान रूप से अपनाया जा सके, तो कोई कारण नहीं कि जिन चमत्कारी ऋद्धि-सिद्धियों को अध्यात्म की परिणति माना जाता है, वे अक्षरशः सही सिद्ध न हों। तीनों की संक्षिप्त विवेचना यहां प्रस्तुत है।
1. उपासना — निकट बैठना। ईश्वर को सर्वतोभावेन आत्म समर्पण करना। उसके निर्देश और अनुशासन को इस सघनता के साथ अपनाना, मानों आग और ईंधन, नाला और नदी एक हो गये हों। एक ने अपनी इच्छा और सत्ता समाप्त कर दी हो और दूसरे में अपने को लय करने में कोई कमी न रखी हो। पूजा-पाठ इसी मनःस्थिति को विनिर्मित करने का एक माध्यम है। अपनाया उसे भी जाय, किन्तु सद्भावनाओं, सत्प्रवृत्तियों का समन्वय ही; विराट् ब्रह्म, विशाल विश्व अर्थात् ईश्वर है उसका कोई नाम रूप नहीं। यह व्यापक सत्ता निराकार ही हो सकती है। फिर भी कोई उसकी इच्छित कल्पना एवं स्थापना अपने मन से कर सकता है। प्रस्तोता उसका नाम गायत्री मंत्र के शब्दों में और सविता-उदीयमान स्वर्णिम सूर्य के रूप में अपनाता रहा है। दूसरे अपनी इच्छानुसार और अन्य नामों-रूपों में भी मान्यता यह सन्निहित कर सकते हैं।
साम्प्रदायिक प्रचलनों, रीति-रिवाजों को भी ईश्वर की वाणी कहते रहे हैं। यह समयानुसार परिवर्तनशील हैं। इसलिए इन्हें भी सामयिक उपयोगिता की कसौटी पर कसते हुए मान्यताओं के रूप में स्थिर किया जा सकता है।
2. ईश्वर प्राप्ति की पात्रता अर्जित करने का दूसरा अवलम्बन है—‘‘साधना’’। अर्थात् जीवन साधना। सधा हुआ संयमी जीवन। मानवी गरिमा के अनुरूप क्रियाओं, मर्यादाओं का अवलम्बन और वर्जनाओं का निरस्त्रीकरण, सभ्यता एवं सुसंस्कारिता की अवधारणा। उत्कृष्ट आदर्शवादिता के अनुशासनों का अवधारण। संचित कुसंस्कारों का गुण, कर्म, स्वभाव से निष्कासन। देवमानव स्तर के गुण, कर्म, स्वभाव का अवलम्बन, अभिवर्धन। सरकस के जानवरों जैसा आत्मशिक्षण, सुरम्य उद्यान स्तर का सुनियोजित जीवन यापन। संस्कारों को पवित्र बनाने वाली यही साधना है। तपश्चर्या की, संयम साधना से तुलना इसी कारण की जाती है।
3. आराधना अर्थात् उदारता। देने में प्रसन्नता। लेने में संकोच। सादा-जीवन, उच्च-विचार। न्यूनतम में निर्वाह। बचत का सर्वतोमुखी सुसंस्कारिता के लिए नियोजन। गिरों को उठाने और उठों को उछालने में अभिरुचि। इसी को पुण्य-परमार्थ कहा जाता है। दान की परम्परा यही है। वसुधैव कुटुम्बकम् और आत्मवत् सर्वभूतेषु के दोनों सिद्धान्त इसी आधार पर विनिर्मित हैं। धर्म-धारणा और सेवा-साधना का निर्वाह भी आराधना के अन्तर्गत आता है। देवत्व की प्रवृत्ति एवं रीति-नीति भी यही है।
अध्यात्म तत्त्वज्ञान उपासना, साधना, आराधना के समन्वय पर अवलम्बित है। इन तीनों को जीवनचर्या की हर क्रिया-प्रक्रिया के साथ जोड़ना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि इसके विपरीत तो कुछ नहीं बन पड़ रहा है?
आराधना का एक पक्ष है—शुभ का संवर्धन और दूसरा है—अशुभ का उन्मूलन। इन्हें सहयोग और संघर्ष के नाम से जाना जाता है।
बोने और काटने का सिद्धान्त आराधना-विज्ञान के अन्तर्गत ही आता है। न्याय-निष्ठा एवं औचित्य का नीर-क्षीर विवेक भी आराधना का ही एक भाग है।
पात्रता अर्जित करने के लिए उपासना, साधना और आराधना के त्रिविध प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर आत्मिक स्वस्थता बन पड़ती है। पूजन, अर्चन, उपहार आदि क्रिया-कृत्यों को भी आत्म-साधना का अंग माना जाता है; पर वह ऐसा ही है, जैसा कि स्वस्थ शरीर पर धुले वस्त्र और श्रृंगार-साधनों की सुसज्जा। आवश्यकता उसकी भी है, पर उसे महत्त्व इतना ही देना चाहिए, जितना कि अपेक्षित है। पूजा-कृत्यों को यदि काय-कलेवर और आत्म-साधना को यदि प्राण-कलेवर समझा जाय, तो भी ठीक है। दोनों के बीच अविच्छिन्न संबंध है। पूर्णता तक पहुंचने के लिए जीवन-शोधन ही वह तत्त्व है, जिसे भक्ति-भावना की जड़ों के सहारे और आगे बढ़ाया जाता है।
इन पंक्तियों के लेखक द्वारा भूत-काल में जो सफलताएं पायी गई हैं, वर्तमान में जो योजनाएं बनाई गयी हैं और भविष्य के लिए जो तैयारियां की गयी हैं। उनकी सफलताओं का रहस्य इस एक ही केन्द्र पर केन्द्रित समझा जा सकता है कि उसने आत्म परिष्कार के उपरोक्त तीनों आधारों को समग्र निष्ठा के साथ अपनाया है। इस संदर्भ में अन्य सफलता प्राप्ति के इच्छुकों को भी इसी समग्रता का अनुकरण करना चाहिए।
इन दिनों विज्ञान और बुद्धिवाद की अभिवृद्धि ने सुविधा-साधनों के अम्बार खड़े कर दिये हैं। पूर्वजों की तुलना में भौतिक दृष्टि से हम कहीं सुविधासम्पन्न हैं। सम्पदा की उपलब्धि को यदि प्रगति कहा जाय, तो मानना पड़ेगा कि पूर्वजों की तुलना में हम कहीं आगे हैं; पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। जनसाधारण का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह गड़बड़ा रहा है। दुर्बलता और रुग्णता दिन-दिन तूफानी गति से बढ़ती जा रही है। अस्पताल, डॉक्टर और औषधि आविष्कारों ने हमें स्वस्थ और समर्थ बनाने में कोई सहायता नहीं की है, कारण कि आहार-विहार में बढ़ा हुआ असंयम, स्वस्थ जीवन के मूलभूत आधार को ही नष्ट किये दे रहा है। पैसा बढ़ा है; पर उसके साथ ही दुर्व्यसनों और प्रदर्शनों के निमित्त होने वाले अपव्यय की इतनी वृद्धि हुई है कि हर कोई अपने को अभावग्रस्त अनुभव करता है। कामचोरी, हरामखोरी को प्रश्रय मिलते रहने पर किसी भी क्षेत्र में वास्तविक एवं अभीष्ट प्रगति हो नहीं सकती। गुण, कर्म, स्वभाव में घुसे हुए दुर्गुण आये दिन ऐसे संकट खड़े करते रहेंगे, जिनका समाधान करने में भौतिक उपचार एवं अनुदान कुछ काम न आ सकें। बढ़ते हुए अविश्वास, असहयोग, अनाचार के पीछे चरित्र-भ्रष्टता ही मूल कारण है। क्रोध से क्रोध और अनाचार से अनाचार बढ़ता है। यह विपन्नता आज संसार के समूचे जलाशय पर जलकुम्भी-काई की तरह छायी दीखती है और जलाशय से मिलने वाले लाभों का अन्त हो रहा है। पथभ्रष्ट को किस प्रकार कंटीली झाड़ियों से संत्रस्त होना पड़ता है, इसे हममें से प्रत्येक को सर्वत्र घटित होते देखा जा सकता है।
प्रदूषण, विकिरण, पर्यावरण, अपराध, छल आदि के जो संकट व्यापक रूप से घहरा रहे हैं, उनकी परिणति की कल्पना और चिन्ताजनक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक साधन जुटा सकना कठिन प्रतीत होता है। अवांछनीयता और वातावरण में संव्याप्त विपन्नता कैसे पनपी? इसका उत्तर वस्तुओं की कमी होने की बात कहने से नहीं मिल सकता। मानना यही पड़ेगा कि विचार क्षेत्र में बढ़ती हुई उद्दण्डता का, आपाधापी का प्रदूषण ही उन समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, जो अप्रसन्नता और अव्यवस्था का निमित्त कारण बनी हुई हैं।
संक्षेप में यही निष्कर्ष निकलता है कि नीतिनिष्ठा और समाजनिष्ठा के आदर्शों की अवहेलना करने पर ही समूचा मनुष्य समुदाय उस विपत्ति में फंसा है, जिससे निकलना और उबरना असंभव नहीं, तो कम से कम सहज तो प्रतीत नहीं होता है। आशा की किरण एक ही है—लोकमानस का परिष्कार, आदर्शों का परिपालन, विचारों का परिशोधन, चरित्र और प्रयासों में आदर्शों का सम्पुट लगाया जाना। उनके बिना प्रस्तुत असंख्यों समस्याओं में से एक का भी सीधा समाधान मिलना नहीं है।
उक्त महान प्रयोजन की पूर्ति अध्यात्म तत्त्वज्ञान से होती है। भावनाओं और मान्यताओं का उदात्तीकरण इसी आधार पर संभव है। प्रस्तुत विश्व-समस्याओं का निराकरण भी यही है। व्यक्तियों को भ्रान्तियों एवं अवांछनीयताओं से मुक्त करके ही उन्हें मौज से रहने और रहने देने की स्थिति में लाया जा सकता है। हंसती-हंसाती जिन्दगी, मिल-बांटकर खाने की प्रवृत्ति, झपटने-हड़पने की अपेक्षा सेवा-सहायता में रुचि लेने की रीति-नीति ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बना सकती है और उन सारी विपत्तियों से एकबारगी छुटकारा दिला सकती है, जिनके कारण कि महाविनाश की आशंका पनप रही है।
उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्रचलित भाषा में जिसे ‘‘विचार क्रान्ति’’ कहा जाता है और पुरातन सोच के अनुसार जनमानस का परिष्कार कहा जा सकता है। इस मर्यादा को अन्तःकरण की गहराई तक पहुंचाने में मात्र अध्यात्म तत्त्वदर्शन ही समर्थ हो सकता है। इस प्रकार समर्थ एवं प्रखर अध्यात्म से ही यह आशा की जा सकती है कि व्यक्ति और समाज के सामने प्रस्तुत असंख्यों विपन्नताओं-विभीषिकाओं का समाधान हो सकेगा।
इसके अतिरिक्त वह शक्ति भी जीवन्त अध्यात्म में ही है, जो सर्वतोमुखी समर्थता और प्रगतिशीलता से जनसाधारण को लाभान्वित कर सके। अध्यात्म की चर्चा सिद्धियों के संबंध में भी होती रहती है और कहा जाता रहा है कि सतयुग की वापसी जैसा सुखद वातावरण यदि उससे विनिर्मित करना हो, तो मनुष्य को समझना और समझाना पड़ेगा कि जिस प्रकार शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल, कौशल बल आदि के सम्पादन का प्रयत्न किया जाता रहा है, उससे बढ़कर आत्म बल का उपार्जन-अभिवर्धन होना चाहिए। उज्ज्वल भविष्य की संरचना इसी आधार पर हो सकेगी। इक्कीसवीं सदी में जिन सुखद भवितव्यताओं की अपेक्षा की जा रही है, उसके लिए दैवी शक्ति के रूप में अध्यात्म का सर्वतोमुखी संवर्धन होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता एवं दूरदर्शिता यही है।
कठिनाई यह है कि परिस्थितियों को देखते हुए अध्यात्म के संबंध में इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो चली है। भौतिक विज्ञान और प्रच्छन्न अध्यात्म ने मिल-जुलकर ऐसा वातावरण बनाया है, जिससे श्रद्धा डगमगाती है और आत्म-साधना का कोई जल्दबाजी भरा परिणाम न आने से उस ओर सर्वसाधारण की प्रवृत्ति को मोड़ना अतिशय कठिन हो रहा है।
वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच बने रहस्य उद्घाटित करने के लिए दैवी-नियोजन ने सर्वसाधारण के सामने एक सुयोग प्रस्तुत किया है। शान्तिकुंज की भूतकालीन गतिविधियों में यदि कुछ आनंददायक और उत्साहवर्द्धक है, तो उसका श्रेय आत्म-शक्ति को ही जाता है। भले ही प्रयोक्ता कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो। भूतकाल में सभी का उल्लेख हो चुका। इन दिनों जो तैयारी चल रही है, उसे भी इसी स्तर का समझा जा सकता है कि कोई सर्वशक्तिमान नियोजन कार्यान्वित होने जा रहा है। उसे भी इस भाषा में कहा जा सकता है, मानों कोई सत्ता असंभव को संभव करने जा रही हो।
युग परिवर्तन के भूतकालीन, आज के और भावी प्रयत्नों को जोड़कर देखा जाय, तो इसे ‘‘आत्म शक्ति से समाज संरचना’’ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इतने पर भी पूर्व असमंजस जहां का तहां अड़ा रह जाता है कि बात यदि ऐसी है, तो इतने बड़े समुदाय द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया अपने द्वारा किसी महत्त्वपूर्ण संरचना का परिचय क्यों नहीं दे रही है?
यह साधारण असमंजस नहीं है। इसके निराकरण के ऐसे समाधानकारक प्रमाण चाहिए, जो अविश्वास को विश्वास में बदल सकें। साथ ही यह रहस्योद्घाटन भी कर सकें कि सशक्त और सही अध्यात्म का स्वरूप क्या हो सकता है, जो अपनी प्रखरता का परिचय दे सके; और साथ ही इस तथ्य से भी सर्वसाधारण को अवगत कराया जाना चाहिए कि वे अभाव क्या हैं, जिनकी उपेक्षा के कारण पूजा-पत्री और कथा-वार्ता मात्र विडम्बना बनकर रह गयीं। दिग्भ्रान्त लोगों को इसी कारण से ऐसी असफलताएं हस्तगत हुईं, जो न केवल उसको असमर्थ और उपहासास्पद बनाती रहीं, वरन् लोक श्रद्धा भी डगमगाती रही, विचारशीलों को उस उत्साह से वंचित भी करती रही, जिससे कि वे सही दिशाधारा अपनाकर अपने को और अपने समूचे समूह को कृत-कृत्य बनाते।
इन समस्त समाधानों के लिए शान्तिकुंज के संचालक द्वारा निजी जीवन में अपनाये गये उन तथ्यों पर प्रकाश डालना पड़ रहा है, जिसमें वे भूतकाल को साक्षी रूप में प्रस्तुत करते हुए, वर्तमान क्रिया-कलापों के औचित्य पर विश्वास करने की मनःस्थिति पैदा कर सकते हैं। साथ ही भावी योजना के लिए जितनी जनशक्ति और साधनशक्ति की अपेक्षा होगी, उसे सफल-सम्पन्न कर सकते हैं। इससे शक्ति-संचय हेतु किये गये पुरुषार्थ और तदनुरूप दैवी अनुकम्पा के सहयोग की सम्भावना का रहस्य आसानी से समझा जा सकता है।
प्रस्तोता ने पूजा-अर्चा की उपेक्षा की हो, सो बात नहीं। इस दिशा में सघन विश्वासी जो कर सकता है, वह भी उनने दुस्साहस स्तर पर पूरा किया है। पर साधना को ही उन प्रयोगों में भी अपनाया है, जिन्हें अध्यात्म का प्राण कहा जा सकता है।
कपड़े को धोने के बाद ही उस पर रंग चढ़ता है। लोहा तो भट्टी में गलने के उपरान्त ही उससे अभीष्ट स्तर के उपकरण ढलने योग्य बन पाता है। पात्रता के अनुरूप ही अनुदान मिलते हैं। इन उदाहरणों की चर्चा इस संदर्भ में की जा रही है कि अध्यात्मवादी को निजी व्यक्तित्व के परिष्कार को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसकी शोभा-सज्जा के लिए जप-तप को प्रश्रय देना चाहिए। यही है प्रयोक्ता का अनुभव और प्रतिदान, जो साक्षी रूप में इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिसने इस दिशा में चलने का साहस जुटा लिया है, उसे यह भी जानना चाहिए कि समग्र साधना-सम्पादन के लिए किन तथ्यों को अविस्मरणीय मानते हुए अपनाने की तैयारी करनी चाहिए।
इन पंक्तियों के लेखक ने अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों की प्रेरणा, अनुसंधान, अनुभव के आधार पर यह जाना और माना है कि आत्म विज्ञान की त्रिवेणी संगम की तरह तीन दिशा धाराएं हैं:— (1) उपासना (2) साधना (3) आराधना। तीनों के समन्वय से ही एक पूरी बात बनती है।
मनुष्य अन्न, पानी और हवा के आधार पर जीता है। तीन लोक प्रसिद्ध हैं। तीन देवता प्रमुख कहे गये हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य समय के तीन काल माने जाते हैं। जीव, ईश्वर और प्रकृति के समन्वय से संसार चल रहा है। इसी प्रकार यह भी माना जाना चाहिए कि (1) उपासना (2) साधना (3) आराधना का समन्वय ही आत्मशक्ति के उपार्जन को सुनिश्चित करता है। इन्हें समान रूप से अपनाया जा सके, तो कोई कारण नहीं कि जिन चमत्कारी ऋद्धि-सिद्धियों को अध्यात्म की परिणति माना जाता है, वे अक्षरशः सही सिद्ध न हों। तीनों की संक्षिप्त विवेचना यहां प्रस्तुत है।
1. उपासना — निकट बैठना। ईश्वर को सर्वतोभावेन आत्म समर्पण करना। उसके निर्देश और अनुशासन को इस सघनता के साथ अपनाना, मानों आग और ईंधन, नाला और नदी एक हो गये हों। एक ने अपनी इच्छा और सत्ता समाप्त कर दी हो और दूसरे में अपने को लय करने में कोई कमी न रखी हो। पूजा-पाठ इसी मनःस्थिति को विनिर्मित करने का एक माध्यम है। अपनाया उसे भी जाय, किन्तु सद्भावनाओं, सत्प्रवृत्तियों का समन्वय ही; विराट् ब्रह्म, विशाल विश्व अर्थात् ईश्वर है उसका कोई नाम रूप नहीं। यह व्यापक सत्ता निराकार ही हो सकती है। फिर भी कोई उसकी इच्छित कल्पना एवं स्थापना अपने मन से कर सकता है। प्रस्तोता उसका नाम गायत्री मंत्र के शब्दों में और सविता-उदीयमान स्वर्णिम सूर्य के रूप में अपनाता रहा है। दूसरे अपनी इच्छानुसार और अन्य नामों-रूपों में भी मान्यता यह सन्निहित कर सकते हैं।
साम्प्रदायिक प्रचलनों, रीति-रिवाजों को भी ईश्वर की वाणी कहते रहे हैं। यह समयानुसार परिवर्तनशील हैं। इसलिए इन्हें भी सामयिक उपयोगिता की कसौटी पर कसते हुए मान्यताओं के रूप में स्थिर किया जा सकता है।
2. ईश्वर प्राप्ति की पात्रता अर्जित करने का दूसरा अवलम्बन है—‘‘साधना’’। अर्थात् जीवन साधना। सधा हुआ संयमी जीवन। मानवी गरिमा के अनुरूप क्रियाओं, मर्यादाओं का अवलम्बन और वर्जनाओं का निरस्त्रीकरण, सभ्यता एवं सुसंस्कारिता की अवधारणा। उत्कृष्ट आदर्शवादिता के अनुशासनों का अवधारण। संचित कुसंस्कारों का गुण, कर्म, स्वभाव से निष्कासन। देवमानव स्तर के गुण, कर्म, स्वभाव का अवलम्बन, अभिवर्धन। सरकस के जानवरों जैसा आत्मशिक्षण, सुरम्य उद्यान स्तर का सुनियोजित जीवन यापन। संस्कारों को पवित्र बनाने वाली यही साधना है। तपश्चर्या की, संयम साधना से तुलना इसी कारण की जाती है।
3. आराधना अर्थात् उदारता। देने में प्रसन्नता। लेने में संकोच। सादा-जीवन, उच्च-विचार। न्यूनतम में निर्वाह। बचत का सर्वतोमुखी सुसंस्कारिता के लिए नियोजन। गिरों को उठाने और उठों को उछालने में अभिरुचि। इसी को पुण्य-परमार्थ कहा जाता है। दान की परम्परा यही है। वसुधैव कुटुम्बकम् और आत्मवत् सर्वभूतेषु के दोनों सिद्धान्त इसी आधार पर विनिर्मित हैं। धर्म-धारणा और सेवा-साधना का निर्वाह भी आराधना के अन्तर्गत आता है। देवत्व की प्रवृत्ति एवं रीति-नीति भी यही है।
अध्यात्म तत्त्वज्ञान उपासना, साधना, आराधना के समन्वय पर अवलम्बित है। इन तीनों को जीवनचर्या की हर क्रिया-प्रक्रिया के साथ जोड़ना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि इसके विपरीत तो कुछ नहीं बन पड़ रहा है?
आराधना का एक पक्ष है—शुभ का संवर्धन और दूसरा है—अशुभ का उन्मूलन। इन्हें सहयोग और संघर्ष के नाम से जाना जाता है।
बोने और काटने का सिद्धान्त आराधना-विज्ञान के अन्तर्गत ही आता है। न्याय-निष्ठा एवं औचित्य का नीर-क्षीर विवेक भी आराधना का ही एक भाग है।
पात्रता अर्जित करने के लिए उपासना, साधना और आराधना के त्रिविध प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर आत्मिक स्वस्थता बन पड़ती है। पूजन, अर्चन, उपहार आदि क्रिया-कृत्यों को भी आत्म-साधना का अंग माना जाता है; पर वह ऐसा ही है, जैसा कि स्वस्थ शरीर पर धुले वस्त्र और श्रृंगार-साधनों की सुसज्जा। आवश्यकता उसकी भी है, पर उसे महत्त्व इतना ही देना चाहिए, जितना कि अपेक्षित है। पूजा-कृत्यों को यदि काय-कलेवर और आत्म-साधना को यदि प्राण-कलेवर समझा जाय, तो भी ठीक है। दोनों के बीच अविच्छिन्न संबंध है। पूर्णता तक पहुंचने के लिए जीवन-शोधन ही वह तत्त्व है, जिसे भक्ति-भावना की जड़ों के सहारे और आगे बढ़ाया जाता है।
इन पंक्तियों के लेखक द्वारा भूत-काल में जो सफलताएं पायी गई हैं, वर्तमान में जो योजनाएं बनाई गयी हैं और भविष्य के लिए जो तैयारियां की गयी हैं। उनकी सफलताओं का रहस्य इस एक ही केन्द्र पर केन्द्रित समझा जा सकता है कि उसने आत्म परिष्कार के उपरोक्त तीनों आधारों को समग्र निष्ठा के साथ अपनाया है। इस संदर्भ में अन्य सफलता प्राप्ति के इच्छुकों को भी इसी समग्रता का अनुकरण करना चाहिए।
Write Your Comments Here:
- इस बार का वसन्त पर्व एवं उसकी उपलब्धियां
- माथा-पच्ची निरर्थक नहीं गई
- तपने और तपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- हम बिछड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं
- अध्यात्म अविश्वस्त सिद्ध हुआ तो?
- प्रगति के त्रिविध अवलम्बन
- समय-सम्पदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग
- यह सरल है, कठिन नहीं
- प्रगति के चार चरण
- युग चेतना का प्रसारण
- सत्संग-प्रशिक्षण एवं संगठन
- महान लक्ष्य की विकेन्द्रीकरण योजना
- तीर्थ-प्रक्रिया का पुनर्जीवन
- सृजन शिल्पियों का समर्थ शिक्षण
- दीप यज्ञों की अति सरल एवं अत्यंत प्रेरक प्रक्रिया
- महिलाओं की महानता उभरे
- सहस्रकुण्डी महायज्ञों का देशव्यापी सरंजाम
- युग प्रतिभाएं इस तरह आगे आयें
- शोष जीवन का उत्सर्ग