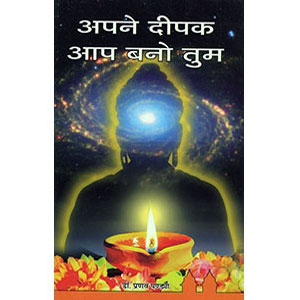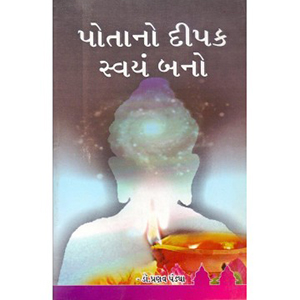अपने दीपक आप बनो तुम 
बहिरंग नहीं, प्रभु के अंतरंग को जाना
Read Scan Version
‘भिक्षां देहि’- सुनकर सुनने वालों के पांव ठिठक गए। करूणा, कोमलता और मधुरता में सने थे ये शब्द। नगर वीथी से गुजर रहे लोगों की अनगिन आँखें उस मुखड़े पर जा टिकीं, जहाँ से ये शब्द निकले थे। तप से दपदप दमकता चेहरा, सरलता का सलोनापन, अजस्र करूणा
की स्रोत आँखें, भव्य देहयष्टि, सचमुच ही सौन्दर्य का सरस पुञ्ज
लग रहे थे, भगवान् तथागत। उनके इस सम्मोहक सौन्दर्य को जिसने भी
देखा- देखता ही रह गया। भगवान् के आगे बढ़ते पाँवों के साथ
अनगिनत मन लिपटे हुए जा रहे थे। सभी की यही चाहत थी कि प्रभु
आज मेरे द्वार रूकें। मेरे यहाँ से भिक्षा ग्रहण करें। मेरा आंगन भगवान् की चरण धूलि से पवित्र हो।
अनेकों के आकर्षण से असंपृक्त प्रभु एक द्वार पर जा रूके। यह श्रावस्ती नगरी के परम विद्वान् वसुबन्धु का घर था। आचार्य वसुबन्धु की गणना नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में की जाती थी। आचार्य विद्वान् होने के साथ अचारवान व तपस्वी थे। उनके घर में केवल तीन प्राणी थे, वे स्वयं, उनकी धर्मपत्नी सुलक्षणा एवं इकलौता युवा पुत्र वक्कलि। प्रभु द्वारा की गयी भिक्षा की पुकार को सबसे पहले उसी ने सुना। और सुनते ही भागा- भागा द्वार पर गया और प्रभु के अद्भुत सौन्दर्य को निहारता ही रह गया। बहुत देर बाद भी जब पुत्र न लौटा तो गृहस्वामी ने पुकारा- बाहर कौन है पुत्र।
इस प्रश्र का भी जब कोई उत्तर न मिला तो स्वयं आचार्य वसुबन्धु द्वार पर आये। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान् तथागत द्वार पर खड़े हैं। यह देखते ही आचार्य हर्ष से विह्वल हो गये। उनका अहोभाव आँखों में छलक आया। गद्गद कण्ठ से उन्होंने कहा- मैं बड़भागी हूँ प्रभु! जो आप मेरे घर आए।
आचार्य वसुबन्धु की सघन श्रद्धा की कड़ियों को सुलझाते हुए प्रभु ने कहा- मैं भिक्षा प्रार्थी हूँ आचार्य। भगवान् के इन वचनों के साथ ही वसुबन्धु ने उनके चरण पखारे और भोजन के लिए आसन पर बिठाया। गृहस्वामिनी सुलक्षणा ने उनको प्रीति व सत्कारपूर्वक भोजन कराया।
तथागत जितनी देर भोजन करते रहे, आचार्य का युवा पुत्र वक्कलि उन्हें एकटक देखता रहा। प्रभु को इस तरह निहारते हुए उसने सोचा कि कितने सम्मोहक हैं भगवान्। यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊँ, तो सदा इन्हें देख पाऊँगा। उसने अपने मन की इस चाहत का छोटा सा अंश अपने माता- पिता को बताया। उसके माता- पिता धर्मपरायण होने के साथ परम विवेकी भी थे। उन्हें संसार की असारता का ज्ञान था। पुत्र भगवान् बुद्ध की शरण में यदि जाना चाहता है, तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या होगा? उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुत्र को भिक्षु होने की अनुमति दे दी।
धम्मं शरणं गच्छामि! संघं शरणं गच्छामि!! बुद्धं शरणं गच्छामि!!! इन तीन प्रतिज्ञाओं के साथ वक्कलि ने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। हालांकि इन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने केवल मुख से उच्चारित किया था। उनका अन्तर्मन तो केवल भगवान् के सौन्दर्य में उलझा हुआ था। वह तो केवल उन्हें देखने के लिए, देखते रहने के लिए प्रवजित हुए थे। यही वजह थी कि वे प्रव्रज्या के दिन से ही ध्यान- धारणा आदि न करके केवल तथागत के रूप- सौन्दर्य को देखा करते थे। प्रारम्भ में भगवान् भी उनके ज्ञान की अपरिपक्वता को देखकर कुछ नहीं कहते थे।
परन्तु जब यह सिलसिला निरन्तर चलता रहा तो प्रभु ने एक दिन वक्कलि को टोका। उसे चेताते हुए उन्होंने कहा- वक्कलि! इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? शरीर तो बस मल- मूत्र का पिटारा है। इसे देखते रहना छोड़कर तुम ध्यान करने की कोशिश करो। धर्म के तत्त्व को जानने की कोशिश करो। धर्म मेरा वास्तविक स्वरूप है। जो धर्म को देखता है, वही मुझे देखता है। भगवान् के इस तरह समझाने के बावजूद वक्कलि को सुध न आयी। उनकी सभी आदतें पहले की ही भाँति बनी रही। वे शास्ता का साथ छोड़कर कहीं भी न जाते थे। शास्ता के कहने पर भी नहीं। किसी भी भाँति उनका यह मोह छूटता ही नहीं था।
उन्हें इस भाँति मोहासक्त देखकर भगवान् ने विचार किया कि यह भिक्षु चोट खाए बिना नहीं सम्हलेगा। यह संवेग को प्राप्त हो, तो ही शायद समझे, सम्हले। सो एक दिन किसी विशिष्ट महोत्सव के समय भगवान् ने उस पर करारी चोट की। हजारों भिक्षुओं के सामने उन्होंने उसका घोर अपमान किया। उसे डांटते, फटकारते, तिरस्कार करते हुए वह बोले- हट जो वक्कलि, तू मेरे सामने से हट जा। तू नीच है, कुसंस्कारी है, तेरा चित्त विकारों से भरा है। तू मेरे पास रहने योग्य नहीं है। यहाँ से चला जा। इन वचनों के साथ ही प्रभु ने भिक्षुओं को संकेत किया कि वे वक्कलि को यहाँ से बाहर निकाल दें।
करूणामूर्ति प्रभु के इस क्रोध ने सभी को चकित कर दिया। सभी हैरान थे। आखिर ऐसा क्यों किया भगवान् ने। वक्कलि को तो प्रभु की बातों से गहरी चोट लगी। उसका अन्तःकरण हाहाकार कर उठा। उसके क्षुब्ध हृदय में पीड़ा आन्दोलित होने लगी। आखिर उसे चोट भी तो गहरी लगी थी। हालांकि उसने इस गहरी चोट की भी गलत व्याख्या की। अपनी भ्रान्तिवश उसने सोचा कि भगवान् मुझसे क्रुद्ध हैं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है। और जब उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है तो फिर इस जीवन का क्या प्रयोजन? जब मैं उनके सामने निरन्तर बैठकर उनका रूप नहीं निहार सकता, तो फिर ऐसे में मर ही जाना उचित है।
अपनी धुन में ऐसा सोचते हुए वह गृद्धकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। पर्वत के पास पहुँचकर उसने आँसू भरी आँखों से पर्वत को देखा और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। इस तरह चढ़ते हुए अन्धेरा हो गया। और वह शिखर पर जा पहुँचा। उस शिखर से कूदकर वह आत्मघात करना चाहता था। भगवान् का स्मरण करते हुए उसने आत्मघात का अन्तिम निश्चय किया। इस आखिरी क्षण में बस वह कूदने को ही था- कि उस घुप्प अंधेरे में से कोई हाथ उसके कन्धे पर आया। उसने पीछे- मुड़कर देखा। भगवान् सामने खड़े थे। अंधेरी रात्रि में उनकी प्रभा अपूर्व थी। आज प्रभु का स्पर्श भी अलौकिक था। इस स्पर्श ने वक्कलि को नयी चेतना दी थी। सो उसने आज शास्ता की देह नहीं, बल्कि स्वयं शास्ता को देखा। आज उसने धर्म को अपने सामने जीवन्त खड़े देखा। एक नयी प्रीति उसमें उमड़ी- ऐसी प्रीति जो कि बांधती नहीं, मुक्त करती है।
तब भगवान् ने इस अपूर्व अनुभूति के क्षण में यह धम्मगाथा कही-
छिदं सीतं परवकम्म कामे पनुद ब्राह्मण।
संखर रानं खयं अत्वा अकटाञ्ञसि ब्राह्मण॥
हे ब्राह्मण! पराक्रम से तृष्णा के स्रोत को काट दे और कामनाओं को दूर कर दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षण को जानकर तुम अकृत- निर्वाह का साक्षात्कार कर लोगे।
भगवान् द्वारा कही गयी इस गाथा को सुनकर वक्कलि की अन्तर्चेतना निर्वाण के पथ पर मुड़ चली। यह परम सौभाग्य प्रभु की कृपा का सुफल था।
अनेकों के आकर्षण से असंपृक्त प्रभु एक द्वार पर जा रूके। यह श्रावस्ती नगरी के परम विद्वान् वसुबन्धु का घर था। आचार्य वसुबन्धु की गणना नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में की जाती थी। आचार्य विद्वान् होने के साथ अचारवान व तपस्वी थे। उनके घर में केवल तीन प्राणी थे, वे स्वयं, उनकी धर्मपत्नी सुलक्षणा एवं इकलौता युवा पुत्र वक्कलि। प्रभु द्वारा की गयी भिक्षा की पुकार को सबसे पहले उसी ने सुना। और सुनते ही भागा- भागा द्वार पर गया और प्रभु के अद्भुत सौन्दर्य को निहारता ही रह गया। बहुत देर बाद भी जब पुत्र न लौटा तो गृहस्वामी ने पुकारा- बाहर कौन है पुत्र।
इस प्रश्र का भी जब कोई उत्तर न मिला तो स्वयं आचार्य वसुबन्धु द्वार पर आये। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान् तथागत द्वार पर खड़े हैं। यह देखते ही आचार्य हर्ष से विह्वल हो गये। उनका अहोभाव आँखों में छलक आया। गद्गद कण्ठ से उन्होंने कहा- मैं बड़भागी हूँ प्रभु! जो आप मेरे घर आए।
आचार्य वसुबन्धु की सघन श्रद्धा की कड़ियों को सुलझाते हुए प्रभु ने कहा- मैं भिक्षा प्रार्थी हूँ आचार्य। भगवान् के इन वचनों के साथ ही वसुबन्धु ने उनके चरण पखारे और भोजन के लिए आसन पर बिठाया। गृहस्वामिनी सुलक्षणा ने उनको प्रीति व सत्कारपूर्वक भोजन कराया।
तथागत जितनी देर भोजन करते रहे, आचार्य का युवा पुत्र वक्कलि उन्हें एकटक देखता रहा। प्रभु को इस तरह निहारते हुए उसने सोचा कि कितने सम्मोहक हैं भगवान्। यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊँ, तो सदा इन्हें देख पाऊँगा। उसने अपने मन की इस चाहत का छोटा सा अंश अपने माता- पिता को बताया। उसके माता- पिता धर्मपरायण होने के साथ परम विवेकी भी थे। उन्हें संसार की असारता का ज्ञान था। पुत्र भगवान् बुद्ध की शरण में यदि जाना चाहता है, तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या होगा? उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुत्र को भिक्षु होने की अनुमति दे दी।
धम्मं शरणं गच्छामि! संघं शरणं गच्छामि!! बुद्धं शरणं गच्छामि!!! इन तीन प्रतिज्ञाओं के साथ वक्कलि ने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। हालांकि इन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने केवल मुख से उच्चारित किया था। उनका अन्तर्मन तो केवल भगवान् के सौन्दर्य में उलझा हुआ था। वह तो केवल उन्हें देखने के लिए, देखते रहने के लिए प्रवजित हुए थे। यही वजह थी कि वे प्रव्रज्या के दिन से ही ध्यान- धारणा आदि न करके केवल तथागत के रूप- सौन्दर्य को देखा करते थे। प्रारम्भ में भगवान् भी उनके ज्ञान की अपरिपक्वता को देखकर कुछ नहीं कहते थे।
परन्तु जब यह सिलसिला निरन्तर चलता रहा तो प्रभु ने एक दिन वक्कलि को टोका। उसे चेताते हुए उन्होंने कहा- वक्कलि! इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? शरीर तो बस मल- मूत्र का पिटारा है। इसे देखते रहना छोड़कर तुम ध्यान करने की कोशिश करो। धर्म के तत्त्व को जानने की कोशिश करो। धर्म मेरा वास्तविक स्वरूप है। जो धर्म को देखता है, वही मुझे देखता है। भगवान् के इस तरह समझाने के बावजूद वक्कलि को सुध न आयी। उनकी सभी आदतें पहले की ही भाँति बनी रही। वे शास्ता का साथ छोड़कर कहीं भी न जाते थे। शास्ता के कहने पर भी नहीं। किसी भी भाँति उनका यह मोह छूटता ही नहीं था।
उन्हें इस भाँति मोहासक्त देखकर भगवान् ने विचार किया कि यह भिक्षु चोट खाए बिना नहीं सम्हलेगा। यह संवेग को प्राप्त हो, तो ही शायद समझे, सम्हले। सो एक दिन किसी विशिष्ट महोत्सव के समय भगवान् ने उस पर करारी चोट की। हजारों भिक्षुओं के सामने उन्होंने उसका घोर अपमान किया। उसे डांटते, फटकारते, तिरस्कार करते हुए वह बोले- हट जो वक्कलि, तू मेरे सामने से हट जा। तू नीच है, कुसंस्कारी है, तेरा चित्त विकारों से भरा है। तू मेरे पास रहने योग्य नहीं है। यहाँ से चला जा। इन वचनों के साथ ही प्रभु ने भिक्षुओं को संकेत किया कि वे वक्कलि को यहाँ से बाहर निकाल दें।
करूणामूर्ति प्रभु के इस क्रोध ने सभी को चकित कर दिया। सभी हैरान थे। आखिर ऐसा क्यों किया भगवान् ने। वक्कलि को तो प्रभु की बातों से गहरी चोट लगी। उसका अन्तःकरण हाहाकार कर उठा। उसके क्षुब्ध हृदय में पीड़ा आन्दोलित होने लगी। आखिर उसे चोट भी तो गहरी लगी थी। हालांकि उसने इस गहरी चोट की भी गलत व्याख्या की। अपनी भ्रान्तिवश उसने सोचा कि भगवान् मुझसे क्रुद्ध हैं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है। और जब उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है तो फिर इस जीवन का क्या प्रयोजन? जब मैं उनके सामने निरन्तर बैठकर उनका रूप नहीं निहार सकता, तो फिर ऐसे में मर ही जाना उचित है।
अपनी धुन में ऐसा सोचते हुए वह गृद्धकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। पर्वत के पास पहुँचकर उसने आँसू भरी आँखों से पर्वत को देखा और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। इस तरह चढ़ते हुए अन्धेरा हो गया। और वह शिखर पर जा पहुँचा। उस शिखर से कूदकर वह आत्मघात करना चाहता था। भगवान् का स्मरण करते हुए उसने आत्मघात का अन्तिम निश्चय किया। इस आखिरी क्षण में बस वह कूदने को ही था- कि उस घुप्प अंधेरे में से कोई हाथ उसके कन्धे पर आया। उसने पीछे- मुड़कर देखा। भगवान् सामने खड़े थे। अंधेरी रात्रि में उनकी प्रभा अपूर्व थी। आज प्रभु का स्पर्श भी अलौकिक था। इस स्पर्श ने वक्कलि को नयी चेतना दी थी। सो उसने आज शास्ता की देह नहीं, बल्कि स्वयं शास्ता को देखा। आज उसने धर्म को अपने सामने जीवन्त खड़े देखा। एक नयी प्रीति उसमें उमड़ी- ऐसी प्रीति जो कि बांधती नहीं, मुक्त करती है।
तब भगवान् ने इस अपूर्व अनुभूति के क्षण में यह धम्मगाथा कही-
छिदं सीतं परवकम्म कामे पनुद ब्राह्मण।
संखर रानं खयं अत्वा अकटाञ्ञसि ब्राह्मण॥
हे ब्राह्मण! पराक्रम से तृष्णा के स्रोत को काट दे और कामनाओं को दूर कर दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षण को जानकर तुम अकृत- निर्वाह का साक्षात्कार कर लोगे।
भगवान् द्वारा कही गयी इस गाथा को सुनकर वक्कलि की अन्तर्चेतना निर्वाण के पथ पर मुड़ चली। यह परम सौभाग्य प्रभु की कृपा का सुफल था।
Write Your Comments Here:
- पहले सेवा, फिर उपदेश
- शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं
- बुद्धत्व ही जीवन का परम स्रोत
- सत्य प्रकट होता है एकांत मौन में
- बोधि के दिव्यास्त्र से विकारों का हनन
- प्रभु प्रेम की कसौटी, उनका ध्यान
- स्वच्छता-निर्मलता का मर्म
- और, अंगुलिमाल अरिहन्त हो गया
- ध्यान की आँख, विवेक की आँख
- आसक्ति अनंत बार मारती है
- क्रोध छोड़ें, अभिमान त्यागें
- नमामि देवं भवरोग वैद्यम्
- महानिर्वाण की अनुभूति
- जीवन का अपने मूल स्रोत से जा मिलना
- श्रद्धा की परिणति
- गलत प्रव्रज्या में रमण दुःखदायी है
- अहंकार गंदगी है, मल है
- सदगुरु का स्मरण
- मनुष्य अपना स्वामी स्वयं
- प्रभु का सान्निध्य
- अब फिर बज उठे रणभेरी
- वीतराग रेवत की सन्निधि का चमत्कार
- बुद्धत्व के सान्निध्य से जन्मा ब्राह्मणत्व
- मोहजनित भ्रांति से प्रभु ने उबारा
- सच्चा भिक्षु
- जहाँ सत्य है, निश्छलता है, वहीं विजय है
- बन्धन मुक्त ही ब्राह्मण है
- सच्चा ब्राह्मण
- पूर्णा चली पूर्णता की डगर पर
- बहिरंग नहीं, प्रभु के अंतरंग को जाना
- निंदा छोड़ो-ध्यान सीखो