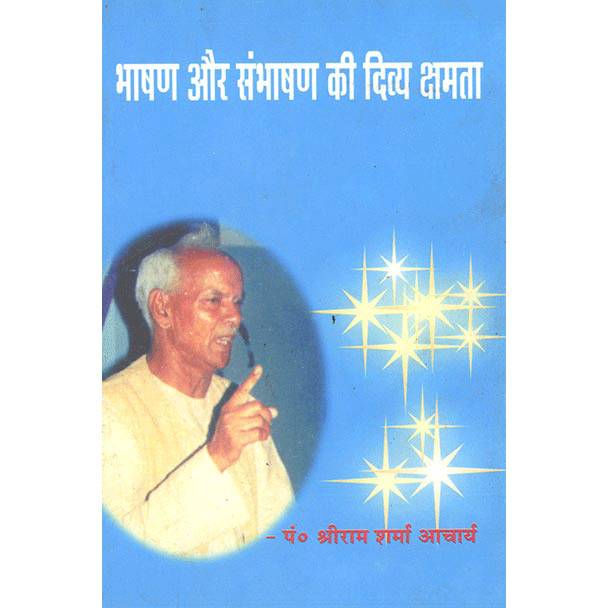भाषण और संभाषण की दिव्य क्षमता 
मात्र भाषण ही नहीं साथ में गायन भी
Read Scan Version
इच्छित उपयोग के लिए बहुत से कला-कौशल सीखे जाते हैं। इस प्रयास में अपनी आजीविका, ख्याति, सुविधा आदि का लाभ उठाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। भाषण कला भी अन्य कला-कौशलों की तरह एक उपजाऊ व्यवसाय है। सेल्समैन, बीमा एजेण्ट, दलाल आदि भाषण तो नहीं करते पर उनकी संभाषण कला में कोई कमी भी नहीं रहती। धर्मोपदेशक, कथा-वाचक एवं चित्र विचित्र आवरण और संस्था संगठनों के संचालक इस कौशल के सहारे ही प्रभुत्व जमाते और प्रकारान्तर से ख्याति और सम्पदा का प्रचुर लाभ अर्जित करते देखे गये हैं। नट, नायकों को भी इसी वाचालता का सहारा लेना पड़ता है। दरबारी प्रकृति के लोग तो इसी के सहारे जीवित रहते हैं। ठग, चमचे, विदूषक, चापलूसों, के लिए तब यह कला ही निर्वाह का माध्यम बनी होती है। यह पुस्तक उनके लिए नहीं लिखी गई है और उन्हें अपने सम्भाषण के साथ किन हथकंडों का समावेश करना होगा इस रहस्योद्घाटन का उल्लेख भी इन पंक्तियों में अभीष्ट नहीं। क्योंकि उस समुदाय को ध्यान में रखते हुए यहां कुछ सोचा विचारा ही नहीं गया। स्वार्थ सिद्धि के लिए किस प्रकार की, किस स्तर की वाचालता अभीष्ट होती है इस सन्दर्भ में पाश्चात्य लेखकों की ढेरों पुस्तकें मण्डी में उपलब्ध हैं। उनकी बिक्री भी लाखों की संख्या में होती है।
यह पुस्तक जन जागृत आत्माओं के लिए लिखी गई है जो नवसृजन के इस पावन पर्व पर युगशिल्पी की भूमिका सम्पन्न करने को उत्सुक हैं, जिन्हें लोकमानस का परिष्कार अभीष्ट है। जो जन-जागरण की बात सोचते हैं और जन-जन के मन-मन में युगान्तरीय चेतना का आलोक उत्पन्न करने में गंभीर हैं। उसके लिए कुछ करने की उत्कण्ठा जिनके भीतर है और जो उसे कार्यान्वित करने में अनिवार्य आवश्यकता की तरह प्रयोग में लाई जाने वाली वाक् सिद्धि का, सरस्वती साधना का अभ्यास करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि उन्हें परिस्थितियों के अनुसार आधारों का अवलम्बन लेना पड़ेगा। अपनी योग्यता को जनता पर लाद नहीं सकेंगे, उन्हें जनता का स्तर देखते हुए अपने को ढालना पड़ेगा।
हर योग्यता के व्यक्ति अपनी क्षमता को अपने स्तर के लोगों के सम्मुख प्रकट करते रहते हैं। तद्नुरूप प्रबन्ध भी हो जाता है। चिकित्सक, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि की अपने-अपने ढंग की ज्ञान गोष्ठियां होती रहती हैं और उनमें उन प्रसंगों में रुचि लेने वाले व्यक्ति इकट्ठे होते रहते हैं। किन्तु नव सृजन के लिए कोई वर्ग विशेष नहीं है। वर्ग है तो उसे एक शब्द में पहचाना जा सकता है—विचारशील, भावनाशील, उदारमना, ऐसे लोग हर वर्ग समुदाय में हो सकते हैं, शिक्षित, अशिक्षित, धनी निर्धन, हिन्दू-मुसलमान आदि किसी भी वर्ग में उन्हें पाया जा सकता है, अपने मन के लोग कहां मिलें जिनमें बीज बोया जाने पर अंकुरित होने की आशा बंधे, तो फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि असली भारत देहात में है। देहात अर्थात् 70 प्रतिशत भारत। यों शहरों में भी अशिक्षितों की कमी नहीं, पर देहात तो उसी वर्ग का अपना क्षेत्र है। देश में 70 प्रतिशत अशिक्षित हैं। इसका विभाजन किया जाय तो शहर का हिस्सा कम और देहात का अधिक होगा। अनुमानतः शहरों में 20 प्रतिशत और देहात में 80 प्रतिशत अशिक्षित माने जा सकते हैं। यही है असली भारत की तस्वीर। हमें इसी समुदाय की सेवा करनी है। उसी को अपना कार्यक्षेत्र मान कर चलना है।
शहरों से अपना कोई द्वेष नहीं। पर उस क्षेत्र में व्यस्तता, लिप्सा, चिन्ता और संकीर्णता का बाहुल्य देखते हुए रचनात्मक कार्यों में सहयोग मिलने की आशा कम ही रखी जा सकती है। फिर उस क्षेत्र पर इतने प्रकार के मत मतान्तर हावी हैं कि खींचतान से दिग्भ्रान्त जैसी स्थिति बन गई है। राजनैतिक संस्थाओं को ही लें। उनका प्रोपेगण्डा बहुत धूमधाम से होता है और दूसरों के विरुद्ध निरन्तर आरोप-आक्षेपों की बौछार-करते रहते हैं। प्रतिपादन इतने सशक्त होते हैं कि सामान्य जन किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते। वे या तो उपेक्षा बरतने लगे हैं या किसी विचार समुदाय के कट्टर अनुयायी बन गये हैं। उनमें भी परिवर्तन तो लाया जाना चाहिए, पर इसके लिए समर्थ तंत्र की आवश्यकता है। उसे मूर्धन्य लोग ही सम्भाल सकते हैं। युग शिल्पियों की प्रतिभा तथा सम्पन्नता इस स्तर की है नहीं कि शहरी जनता को आकर्षित एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक किन्तु अत्यन्त महंगे साधन जुटा सकें। बड़े प्रचार पंडाल के बिना शहरी जनता के प्रभाव सम्मेलन बुला सकना कठिन है। उन साधनों के लिए सुसम्पन्नों की थैलियां कैसे खुले? वे अपने हाथ कैसे लगें? इस विवशता के कारण भी उन खट्टे अंगूरों को नमस्कार करके अपना रास्ता नापना ही उचित है। फिर मूल आवश्यकता भी तो यह कहती है कि शहरों में घुसपैठ की धक्का-मुक्की में पड़ने का कार्य दूसरों पर छोड़ कर हमें अपेक्षित देहातों की ओर मुड़ना और वहां डेरा डालना है। असली भारत दूसरे समाज सेवियों की दृष्टि में नहीं है। वहां साधन-सुविधा के अभाव में बड़े लोग नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंचना चाहते तो उन्हीं का अनुकरण क्यों किया जाय। दूसरे मिशनरियों से भी कुछ क्यों न सीखा जाय, जिनने न केवल, भारत में वरन् संसार के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में अपना डेरा डाला है और देहात के पिछड़े वर्ग को अपना कार्य क्षेत्र चुना है। वहां अशिक्षा, दरिद्रता, अस्वच्छता का बाहुल्य भले ही हो, पर दिग्भ्रान्ति ने अनास्था उत्पन्न नहीं की है। भावना की दृष्टि से इतना कुछ होना बहुत है। इस स्तर की मनोभूमि का सही ढंग से मर्मस्पर्श किया जाय तो वहां प्रकाश और परिवर्तन की प्रक्रिया के फलित होने की अपेक्षाकृत अधिक आशा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हममें से प्रत्येक को अपने सुनिश्चित कार्य क्षेत्र के बारे में निर्भ्रान्त रहना चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए कि उस समुदाय में बौद्धिक आदान-प्रदान के लिए जो सम्भव है उसी उपाय को अपनाया जाय। उनकी आवश्यकता को परिस्थिति की प्रमुखता दी जाय। स्वयं उसके अनुरूप योग्यता उपार्जित करें। अपनी योग्यता उन पर थोपने का हठ न करें।
इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उपरान्त प्रवचन शैली में कथानकों की भरमार करके सुबोध एवं लोकप्रिय स्तर का बनाने का प्रयत्न किया गया है। प्रज्ञा पुराण का सृजन विशुद्ध रूप में इसी निमित्त हुआ है। स्लाइड प्रोजेक्टरों को भी महत्व इसी दृष्टि से दिया गया है कि दिव्य दर्शन कराते हुए उस क्षेत्र की भाषा में युगान्तरीय चेतना को गले उतारने का प्रयत्न किया जाय।
इस संदर्भ में एक पक्ष और भी ध्यान देने योग्य है, वह है—कला के साथ ‘कीर्तन’ का जुड़ा होना। जहां कथा हो वहां कीर्तन अवश्य हो। इस निर्धारण के अनुसार ‘कथा-कीर्तन’ शब्द को अविच्छिन्न बना दिया गया है और दोनों का स्वरूप पृथक-पृथक होते हुए भी उन्हें एक ही श्रृंखला में गूंथ दिया गया है। इसे गद्य और पद्य का समन्वय कहना चाहिए। प्रवचन ही नहीं संगीत भी आवश्यक है। यह इसलिए कि प्रवचन को गले उतारने पर प्रधानतया विचार क्रांति का पथ-प्रशस्त होता है। विचारों को विचारों से टकरा कर अनुपयुक्त चिन्तन छोड़ने और विवेकपूर्ण औचित्य को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। यह आवश्यक है और अनिवार्य भी, पर एक और बात है जिसे भुला नहीं दिया जाना चाहिए। वह है लोकमानस का भावनात्मक परिष्कार। विचारणा और भावना सहेलियां तो हैं, पर उनका अस्तित्व स्वतंत्र भी मानना पड़ेगा। भावना की शक्ति को समझा जाना चाहिए। वह विचारणा से भी अधिक समर्थ है। आदर्शवादी अनुगमन में तो विशुद्ध रूप से भावना की ही भूमिका रहती है। संवेदनाएं ही त्याग बलिदान की उमंगें उत्पन्न करती हैं। करुणा और सेवा का उद्गम भावना क्षेत्र के अन्तराल में ही पाया जाता है। अनास्थाजन्य प्रस्तुत संकट का निराकरण श्रद्धासिक्त उमंगें उभारने से ही बन पड़ेगा’ विचारवान प्रज्ञा इसकी प्रारम्भिक पृष्ठभूमि बनाती है। महामानवों ऋषियों, में अधिकांश भावनाशील थे। बुद्धिमान, विज्ञजन तो चतुरता के धनी ही पाये जाते हैं। वे कथनोपकथन में प्रवीण होते हैं। पर जब त्याग बलिदान का, सत्साहस के प्रकटीकरण का समय आता है तो वह बुद्धिमत्ता ही आड़े आ जाती है जिसके सहारे बड़े-बड़े प्रतिपादन खड़े किये गये थे। यह आक्षेप बहुत हद तक सही है कि बुद्धिमानों से चतुरता, प्रतिभाभर की अपेक्षा करनी चाहिए, वे आदर्शवादिता को चरितार्थ करने वाली-उदार सेना साधना से बचते कतराते ही देखे गये हैं।
यहां विचारणा का महत्व नहीं घटाया जा रहा है कि उस तक सीमित रहने, उस पर निर्भर रहने से बात बनेगी नहीं। भावना क्षेत्र को उमंगाने के लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना होगा। इसके लिए प्रतिपादनों में तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों का समावेश करके ही निश्चित नहीं हो जाना चाहिए वरन् एक कदम और आगे बढ़कर भावनाओं के भण्डार अन्तःकरण का अर्थ स्पर्श करने को महत्व देना चाहिए। हमारे प्रवचन विद्वतापूर्ण ही न हों वरन् उनके रुला देने की भी क्षमता हो। ऐसे आंसू उगाने चाहिए जो करुणा एवं उदारता बनकर सेवा साधना का क्षेत्र सम्हाल सके। आदर्शवादिता की खेती इन्हीं श्याम घटाओं से पनपती है। स्वाति बून्दों जैसा चमत्कार भाव भरी आर्द्रता ही उत्पादन कर सकती है। हमारे प्रतिपादनों में इस संवदना का समुचित समन्वय रहना चाहिए।
इस प्रसंग में एक नया तथ्य सामने आता है—संगीत की शक्ति। कहना न होगा कि जहां तक भाव संवेदना उभारने का प्रश्न है वहां तक प्रवचनों की तुलना में संगीत को कहीं अधिक-शक्तिशाली पाया गया है। सूर, मीरा, चैतन्य आदि की संगीत साधना ने अपने समय में जो चमत्कार उत्पन्न किये उन्हें भुलाया नहीं जा सकता आज भी उनकी संवेदना को जब गीतवाद्य सहित उमंगाया जाता है तो लोग लहराने लगते हैं। दीपक राग बुझे दीपक जलाते थे। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होती थी। वैसी उदाहरण अब देखने को नहीं मिलते और न इन दिनों बहेलिया हिरनों को पकड़ने के लिए वाद्य बजाकर उन्हें मंत्र मुग्ध करते हैं। सपेरे ही सांपों को लहराते देखे जाते हैं। जो हो मनुष्य के भावना क्षेत्र तक प्रवेश पाने के लिए वक्तृता से भी एक कदम आगे बढ़कर संगीत संवेदना का आश्रय लेना होगा। यही कारण है कि कथा के साथ कीर्तन शब्द को अविच्छिन्न किया गया है। गद्य के साथ पद्य का गठबंधन करने से एवं बड़ी अपूर्णता का समाधान निकलता है।
संगीत की तुलना में भावनात्मक क्षेत्र को तरंगित करने वाली शक्ति दूसरी नहीं। शास्त्रकारों ने उसकी महत्ता महिमा ‘‘शब्द ब्रह्म’’ के समतुल्य ही ‘‘नाद ब्रह्म’’ की भी गाई हैं। देवर्षि नारद की वीणा, शंकर का डमरू, कृष्ण की वंशी उनकी आन्तरिक भाव अभिव्यक्तियों का प्रकटीकरण सम्भव बनाती है। नाद योग के द्वारा मिलने वाली सिद्धियों का वर्णन यहां प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। किन्तु उस तथ्य को तो समझना ही होगा कि नव सृजन की उमंगों का उद्भव भावना क्षेत्र से होगा। और उसके लिए संगीत शक्ति को उपेक्षित नहीं रखा जा सकेगा’’ प्रवचन एवं लेखन से सामयिक आवश्यकता की पूर्ति न हो सकेगी। इस त्रिवेणी में गंगा-जमुना की लेखनी वाणी की मूर्खता भले ही रहे पर वीणापाणि सरस्वती की तीसरी धारा का समावेश भी अनिवार्य अपरिहार्य मानकर चलना होगा।
देहात के लिए संगीत की आवश्यकता एवं लोक प्रियता को प्रमुखता देनी होगी। वहां अभी भी अभिव्यक्तियों, भाषणों से नहीं गायनों से ही प्रकट की जाती है। विवाह, शादियों, तीज-त्यौहारों पर महिलाओं को गीत, मल्हार गाते सभी ने सुना है इसके अतिरिक्त आल्हा, ढोला, रामायण—नौटंकी, चौबोला, लावनी, रसिया, बाहरमासी आदि के रूप में गाये जाने वाले लोकगीतों की मंडलियां जुड़ती हैं। जो गा सकते हैं अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। शेष लोग मनोयोगपूर्वक सुनते और रात-रात भर जागते रस लेते देखे जाते हैं। लोक नृत्य समूचे भारत में सर्वत्र प्रचलित हैं। उनके अपने-अपने ढंग और स्वरूप हैं। किन्तु स्मरण रहे-वह संगीत की ही मूक अभिव्यक्ति है। गीत के साथ जो लय तरंगें उद्भूत होती हैं, वे ही कंठ ओष्ठ तक सीमित न रहकर हाथ-पैर गरदन, आंख के चल अवयवों द्वारा थिरकन बनकर फूट पड़ती है। संगीत का समूची काया तथा मनःसंस्थान को तरंगित करने वाला स्वरूप ही नृत्य माना जाता है। ‘ऐक्शन सांग’ इसी की एक मध्यवर्ती अनुकृति है। कीर्तन में पाई जाने वाली भाव-विभोर तन्मयता भी संगीत का ही विकसित एवं विस्तृत स्वरूप है।
स्वर, ताल और अंग संचालन की भाव-विभोरता कितनी मादक होती है और उसकी आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्र में क्या-क्या उपलब्धियां हस्तगत होती हैं—इसकी चर्चा विवेचना इन पंक्तियों में अभीष्ट नहीं। यहां तो इतना ही कहा जा रहा है कि नव-युग की जन-जागरण प्रक्रिया में संगीत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसकी उपयोगिता इस प्रयोजन के लिए उतनी ही है जितनी कि प्रचार पक्ष में काम आने वाले भाषण-संभाषण, लेखन-पठन, आयोजन-आन्दोलन आदि की। प्रत्येक वक्ता को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसे संगीत को साथ लेकर चलना है। प्रवचन के आदि में-अन्त में या दोनों बार संगीत सहगान या कीर्तन का समावेश रखना चाहिए। वह वाद्य यंत्रों की सहायता से बन पड़े तो आकर्षण और भी अधिक बढ़ जायेगा। अन्यथा बिना वादन का गायन भी काम दे सकता है। कथावाचक प्रायः ऐसा करते भी हैं। ‘‘हरे राम हरे कृष्ण.........।’’ ‘‘रघुपति राघव राजाराम.........।’’ ‘‘हे कृष्ण, हे कृष्ण-हरे मुरारे.........।’’ जैसी कितनी ही रामधुनें प्रख्यात हैं। आये दिन नई बनती और पुरानी विस्मृत होती रहती हैं। इन्हें एक बार वक्ता कहता है। दूसरी बार उपस्थित जन-समुदाय दुहराता है। इससे सबका ध्यान एकाग्र होता है। विश्रृंखलता, अस्त-व्यस्तता दूर होकर जागरूकता उत्पन्न होती है और कथन श्रवण का उपक्रम ठीक प्रकार चल पड़ता है।
यह परम्परा का निर्वाह हुआ। बात इतने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोक मानस में अभिनव जागरण एवं उल्लास का समावेश करने के लिए सार्थक, प्रेरणाप्रद एवं भावनाएं तरंगित करने वाले ऐसे गीतों की आवश्यकता है जो युग-चेतना को अग्रगामी बना सकें। ऐसे गीतों को ढूंढ़ने, चयन करने की आवश्यकता न पड़ेगी। उन्हें नये सिरे से लिखा जाना आरम्भ कर दिया गया है और वे बड़ी संख्या में अगले ही दिनों उपलब्ध होने लगेंगे। ‘नये सिरे से’ कहने का एक नया अभिप्राय है कि प्रज्ञा मिशन ने ‘एक ध्वनि’ को मान्यता दी है। उसमें स्वर, ताल और थिरकन इन तीनों का समावेश है। उसकी तर्ज है—
मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धापूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं।। झंकार करो ऐसी सद्भाव उभर आये। हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाये।। सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते हैं। मां तेरे चरणों में..........................।।
इसी एक ध्वनि पर असंख्यों गीत लिख जाने हैं। भिन्नताओं पर रोकथाम इसलिए लगाई गई है कि कवियों को उसी पर लिखने का अभ्यास पड़े। गायकों का गला एक ही प्रयोग पर निरन्तर अभ्यास करते-करते ठीक तरह सध जाय। वादकों के लिए इसमें सबसे अधिक सुगमता है। अनेक ध्वनियों पर वाद्य यंत्रों का अभ्यास करने के लिए स्वर शास्त्र की क्रमबद्ध शिक्षा चाहिए। अनेक सरगम में साधनी और याद करनी पड़ती हैं। स्वर ताल की भिन्नताओं को समझना और उनके अन्तर को अभ्यास में अपनाना पड़ता है, पर जब एक ही लय ध्वनि पर सारा संगीत शास्त्र समाप्त होता है तो फिर सारा झंझट ही मिटा डमरू में कुछ ही बोल निकलते हैं, शंकरजी ने उतने में ही समूह स्वर शास्त्र को केन्द्रित कर लिया तो कोई कारण नहीं कि युग संगीत को एक ध्वनि पर केन्द्रित किया जा सके। इससे गायकों को ही नहीं वादकों को भी भारी सुविधा होगी, वे इस लय का अभ्यास बिना स्वर शास्त्र की सांगोपांवा जानकारी प्राप्त किये एक से दूसरे का अनुकरण करने की विद्या अपना कर-देखते-देखते प्रवीणता प्राप्त कर सकेंगे। इशारे से ही एक साथी अपने दूसरे सहयोगी को अभ्यस्त कर दिया करेगा। कंठ से कंठ मिलाकर गाने भर से गीत क्रम पर गला सूख जाया करेगा।
वाद्य यन्त्रों में यों हारमोनियम, ढोलक, तबला अब सर्वत्र प्रचलित हैं। जहां तक एक ध्वनि का सम्बन्ध है, उन पर भी महीने दो महीने अभ्यास से काम चलाऊ ढर्रा लुढ़कने लग सकता है। महिलाएं बिना कहीं संगीत शिक्षा पाये गीत वादन का काम चलाऊ अभ्यास कर लेती हैं। फिर कोई कारण नहीं कि नियमित एक लय ताल पर सर्व साधारण को अभ्यस्त न बनाया जा सके। प्रचारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कभी पैदल कभी साइकिल पर यही है छोटे देहातों में आवश्यक सामान लेकर पहुंचने का साधन। ऐसी दशा में सफरी बाजे साथ लेकर चलने का उपाय एक ही है। कि हलके वाद्य यंत्र काम में लाये जायें। भावी प्रचार टोलियां दो-दो की होंगी और वे गांव-गांव नव युग का अलख जगाने के लिए परिभ्रमण करेंगी। उनके झोले में ही वाद्य यंत्रों को बिठाना पड़ेगा। इसलिए वे ढपली और मंजीरा-घुंघरू ही हो सकते हैं। लागत कम, वजन कम, घेरा कम, अभ्यास कम-और लाभ अधिक। इस उपाय उपचार का अवलम्बन लेकर गीत और वाद्य दोनों का समन्वय हो सकता है और वक्तृता के समतुल्य ही विचारों की अभिव्यक्ति का-जनजागरण का-एक नया द्वार खुल सकता है।
प्रत्येक युग शिल्पी को कहा गया है कि उसे अपनी वाणी मुखर करनी चाहिए और जन सम्पर्क क्षेत्र में उतर कर जन समर्थन और सहयोग उपलब्ध करने का प्रथम सोपान पूर्ण करना चाहिए। आगे की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापनाओं का द्वार इसी शुभारम्भ से खुलेगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि भाषण को ही समग्र न माना जाय वरन् उसका अविच्छिन्न सहयोगी गायन भी समान अवलम्बन बनाया जाय। वाणी के यह दोनों ही श्रृंगार हैं और अपने-अपने स्थान पर इन दोनों का ही समान उपयोग एवं महत्व है।
कथा प्रसंगों के साथ प्रवचन करने की शैली अत्यधिक सरल और सफल है। उसे शिक्षितों-अशिक्षितों में समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है और चिरकाल तक-एक ही स्थान पर नये-नये संदर्भ सुनाते रहा जा सकता है। दार्शनिक भाषणों की तरह इस प्रक्रिया को अपनाने पर तरकस कभी खाली नहीं होता और शब्द वेधी बाण निशाना बेधने के बाद फिर लौट-लौट कर तरणि को रिक्त नहीं होने देते। प्रज्ञापुराण के बीस खण्ड इसी दृष्टि से सृजे जा रहे हैं कि युग प्रवक्ताओं को अनवरत अमृत वर्षा करते हुए भण्डार चुक जाने की चिन्ता आशंका न करनी पड़े। इसी का समान्तर-सहयोगी-पूरक पथ युग गायन का है। इसे भी समान महत्व मिलना चाहिए और सीखने अपनाने में समान उत्साह रहना चाहिए।
शांति कुंज हरिद्वार में एक-एक महीने के युग शिल्पी सत्रों में भाषण और गायन के दोनों शिक्षणों की दो कक्षाएं साथ-साथ चलती हैं। जिन्हें एक महीना ठहरना है वे दोनों में से एक का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों में प्रवीणता एक साथ इतनी थोड़ी अवधि में नहीं हो सकती। जिन्हें दोनों सीखने हैं उन्हें दो महीने ठहरना पड़ेगा। इतने पर भी यह शर्त रहेगी ही कि छात्रों में इन कला कौशलों की मौलिक प्रतिभा तो रहनी ही चाहिए। जिनका संकोच हीन टूटा, उत्साह हीन उमंगा—वे भाषण कला में प्रवीणता प्राप्त न कर सकेंगे। मुंह खुलना बात दूसरी है और प्रवीणता पाना दूसरी। आजकल सर्वत्र ‘‘ए-वन’’ की मांग है इसे तो सभी जानते हैं। संगीत के बारे में भी यही बात है। गले की बनावट और ताल स्वर को समझने अपनाने की पकड़ तो अभ्यासी में होनी ही चाहिए अन्यथा अध्यापक के लाखों प्रयत्न करने पर भी आशाजनक प्रगति न हो सकेगी। फिर भी न कुछ से कुछ होना अच्छा है। शिक्षण, साधन और अभ्यास के अभाव में असंख्यों को आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। वह कठिनाई तो निश्चित रूप से इन सत्रों में सम्मिलित होने से दूर हो सकती है।
आवश्यक नहीं कि जो सीखना है, सिखाया जाना है उसके लिए हरिद्वार सत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य ही हो। यह कार्य अभ्यस्त लोग अपने साथियों को अभ्यास कराने का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर वहन कर भी पूरा कर सकते हैं। प्रशिक्षित लोग शान्ति कुंज की शैली पर अपने अपने यहां भी भाषण कला के अभ्यास की कक्षाएं चलाते रह सकते हैं और अनेकों को अभ्यस्त एवं प्रवीण बना सकते हैं। यही बात संगीत के सम्बन्ध में भी है। जिन्हें पूर्वाभ्यास है वे निर्धारित लय ध्वनि का घर बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं। नई निर्धारित ध्वनि पर बनने वाले गीतों को मंगाते सीखते और सिखाते रह सकते हैं। सुव्यवस्थित विद्यालयों में तो हारमोनियम, ढोलक, तबला भी सिखाया जा सकता है परन्तु जहां उतने साधन न हों, समय का अभाव हो, जिन्हें चलते फिरते प्रचार करना हो उनके लिए ढपली, मजीरा, घुंघरू इन दो स्वल्प व्यय साध्य, स्वल्प समय साध्य वाद्य यंत्रों को बजाना और अभ्यस्त ध्वनि मीटर का निरन्तर प्रयोग करते हुए नवीनता तथा प्रेरणा उभारते रहने का अवसर मिल सकता है।
चलते-फिरते गायन वादन में श्रोता तलाशने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। रेल में, बस में, मुसाफिर खाने में, हाट-बाजार में, धर्मशाला में, प्याऊ पर, घाट, मन्दिर, चौराहे, पार्क के आस पास कहीं भी बैठकर दो व्यक्ति मिल जुलकर ढपली, घुंघरू बजाते हुए मस्ती और प्रेरणा से भरे पूरे गीत गाने लगें तो श्रोताओं की भीड़ बिना किसी पूर्व सूचना या आमंत्रण के देखते-देखते जमा हो सकती है। इस सभा समारोह पर किसी का बंधन प्रतिबंध नहीं। जब इच्छा हुई प्रचार आयोजन आरंभ कर दिया और जब बंद करने की आवश्यकता अनुभव हुई तभी दोनों बाजे थैली में बंद किये, पल्ला झाड़ा और उठ खड़े हुए। न स्वागत की प्रतीक्षा करनी होती है और न विदाई का धन्यवाद लेने की। ढपली, घुंघरू वाला सम्मेलन समारोह ऐसा है जिसे कथा प्रवचन से भी सरल कहा जा सकता है। इसमें शक्ति का व्यय कम से कम, झंझट कम से कम तथा सरलता सुविधा अधिक से अधिक है। देहातों के लिए तो यह प्रक्रिया हर दृष्टि से सरल सफल मानी जायेगी। गीत-वाद्य के साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी व्याख्या विवेचना इतने भर से वह उद्देश्य भली प्रकार पूरा हो जाता है जिसकी पूर्ति के लिए वक्तृत्व कला सीखने सिखाने की सुव्यवस्थित योजना बनायी गयी है।
अगले दिनों साइकिलों पर तीर्थ यात्रा का, भारत भ्रमण का आन्दोलन चल पड़ेगा। युग शिल्पी बादलों की तरह खेत-खेत पर बरसने और सूखे भूखण्डों हरीतिमा लहलहाने का संकल्प लेकर निकलेंगे। गांव-गांव घर-घर, अलख जगाने की पुरातन सन्त परम्परा को पुनर्जीवन प्रदान किया जा रहा है। अपने गांव घर से हरिद्वार-हरिद्वार से दूसरे रास्ते घर पहुंचने की तीर्थ यात्रा को नये उत्साह नयी उमंगों और नयी योजनाओं के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है उसमें प्रज्ञा पुराण की कथा प्रक्रिया उतनी सफल सिद्ध न होगी जितनी कि ढपली घुंघरू के सहारे युग संगीत सुनाये और देखते-देखते श्रोताओं की भीड़ जमाकर लेने की।
कथा प्रवचन का अपना महत्व है और युग संगीत का अपना। हमें दोनों को ही महत्व देना चाहिए और आवश्यकतानुसार दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए। कथा कीर्तन की जोड़ी इसीलिए बनाई गयी है कि मुखरता के दोनों माध्यमों में अभ्यास साथ-साथ चलता रहे। अभिरुचि तथा प्रतिष्ठा को नहीं समय की मांग और लक्ष्य की पूर्ति को प्रमुखता देनी होगी।
यह पुस्तक जन जागृत आत्माओं के लिए लिखी गई है जो नवसृजन के इस पावन पर्व पर युगशिल्पी की भूमिका सम्पन्न करने को उत्सुक हैं, जिन्हें लोकमानस का परिष्कार अभीष्ट है। जो जन-जागरण की बात सोचते हैं और जन-जन के मन-मन में युगान्तरीय चेतना का आलोक उत्पन्न करने में गंभीर हैं। उसके लिए कुछ करने की उत्कण्ठा जिनके भीतर है और जो उसे कार्यान्वित करने में अनिवार्य आवश्यकता की तरह प्रयोग में लाई जाने वाली वाक् सिद्धि का, सरस्वती साधना का अभ्यास करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि उन्हें परिस्थितियों के अनुसार आधारों का अवलम्बन लेना पड़ेगा। अपनी योग्यता को जनता पर लाद नहीं सकेंगे, उन्हें जनता का स्तर देखते हुए अपने को ढालना पड़ेगा।
हर योग्यता के व्यक्ति अपनी क्षमता को अपने स्तर के लोगों के सम्मुख प्रकट करते रहते हैं। तद्नुरूप प्रबन्ध भी हो जाता है। चिकित्सक, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि की अपने-अपने ढंग की ज्ञान गोष्ठियां होती रहती हैं और उनमें उन प्रसंगों में रुचि लेने वाले व्यक्ति इकट्ठे होते रहते हैं। किन्तु नव सृजन के लिए कोई वर्ग विशेष नहीं है। वर्ग है तो उसे एक शब्द में पहचाना जा सकता है—विचारशील, भावनाशील, उदारमना, ऐसे लोग हर वर्ग समुदाय में हो सकते हैं, शिक्षित, अशिक्षित, धनी निर्धन, हिन्दू-मुसलमान आदि किसी भी वर्ग में उन्हें पाया जा सकता है, अपने मन के लोग कहां मिलें जिनमें बीज बोया जाने पर अंकुरित होने की आशा बंधे, तो फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि असली भारत देहात में है। देहात अर्थात् 70 प्रतिशत भारत। यों शहरों में भी अशिक्षितों की कमी नहीं, पर देहात तो उसी वर्ग का अपना क्षेत्र है। देश में 70 प्रतिशत अशिक्षित हैं। इसका विभाजन किया जाय तो शहर का हिस्सा कम और देहात का अधिक होगा। अनुमानतः शहरों में 20 प्रतिशत और देहात में 80 प्रतिशत अशिक्षित माने जा सकते हैं। यही है असली भारत की तस्वीर। हमें इसी समुदाय की सेवा करनी है। उसी को अपना कार्यक्षेत्र मान कर चलना है।
शहरों से अपना कोई द्वेष नहीं। पर उस क्षेत्र में व्यस्तता, लिप्सा, चिन्ता और संकीर्णता का बाहुल्य देखते हुए रचनात्मक कार्यों में सहयोग मिलने की आशा कम ही रखी जा सकती है। फिर उस क्षेत्र पर इतने प्रकार के मत मतान्तर हावी हैं कि खींचतान से दिग्भ्रान्त जैसी स्थिति बन गई है। राजनैतिक संस्थाओं को ही लें। उनका प्रोपेगण्डा बहुत धूमधाम से होता है और दूसरों के विरुद्ध निरन्तर आरोप-आक्षेपों की बौछार-करते रहते हैं। प्रतिपादन इतने सशक्त होते हैं कि सामान्य जन किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते। वे या तो उपेक्षा बरतने लगे हैं या किसी विचार समुदाय के कट्टर अनुयायी बन गये हैं। उनमें भी परिवर्तन तो लाया जाना चाहिए, पर इसके लिए समर्थ तंत्र की आवश्यकता है। उसे मूर्धन्य लोग ही सम्भाल सकते हैं। युग शिल्पियों की प्रतिभा तथा सम्पन्नता इस स्तर की है नहीं कि शहरी जनता को आकर्षित एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक किन्तु अत्यन्त महंगे साधन जुटा सकें। बड़े प्रचार पंडाल के बिना शहरी जनता के प्रभाव सम्मेलन बुला सकना कठिन है। उन साधनों के लिए सुसम्पन्नों की थैलियां कैसे खुले? वे अपने हाथ कैसे लगें? इस विवशता के कारण भी उन खट्टे अंगूरों को नमस्कार करके अपना रास्ता नापना ही उचित है। फिर मूल आवश्यकता भी तो यह कहती है कि शहरों में घुसपैठ की धक्का-मुक्की में पड़ने का कार्य दूसरों पर छोड़ कर हमें अपेक्षित देहातों की ओर मुड़ना और वहां डेरा डालना है। असली भारत दूसरे समाज सेवियों की दृष्टि में नहीं है। वहां साधन-सुविधा के अभाव में बड़े लोग नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंचना चाहते तो उन्हीं का अनुकरण क्यों किया जाय। दूसरे मिशनरियों से भी कुछ क्यों न सीखा जाय, जिनने न केवल, भारत में वरन् संसार के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में अपना डेरा डाला है और देहात के पिछड़े वर्ग को अपना कार्य क्षेत्र चुना है। वहां अशिक्षा, दरिद्रता, अस्वच्छता का बाहुल्य भले ही हो, पर दिग्भ्रान्ति ने अनास्था उत्पन्न नहीं की है। भावना की दृष्टि से इतना कुछ होना बहुत है। इस स्तर की मनोभूमि का सही ढंग से मर्मस्पर्श किया जाय तो वहां प्रकाश और परिवर्तन की प्रक्रिया के फलित होने की अपेक्षाकृत अधिक आशा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हममें से प्रत्येक को अपने सुनिश्चित कार्य क्षेत्र के बारे में निर्भ्रान्त रहना चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए कि उस समुदाय में बौद्धिक आदान-प्रदान के लिए जो सम्भव है उसी उपाय को अपनाया जाय। उनकी आवश्यकता को परिस्थिति की प्रमुखता दी जाय। स्वयं उसके अनुरूप योग्यता उपार्जित करें। अपनी योग्यता उन पर थोपने का हठ न करें।
इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उपरान्त प्रवचन शैली में कथानकों की भरमार करके सुबोध एवं लोकप्रिय स्तर का बनाने का प्रयत्न किया गया है। प्रज्ञा पुराण का सृजन विशुद्ध रूप में इसी निमित्त हुआ है। स्लाइड प्रोजेक्टरों को भी महत्व इसी दृष्टि से दिया गया है कि दिव्य दर्शन कराते हुए उस क्षेत्र की भाषा में युगान्तरीय चेतना को गले उतारने का प्रयत्न किया जाय।
इस संदर्भ में एक पक्ष और भी ध्यान देने योग्य है, वह है—कला के साथ ‘कीर्तन’ का जुड़ा होना। जहां कथा हो वहां कीर्तन अवश्य हो। इस निर्धारण के अनुसार ‘कथा-कीर्तन’ शब्द को अविच्छिन्न बना दिया गया है और दोनों का स्वरूप पृथक-पृथक होते हुए भी उन्हें एक ही श्रृंखला में गूंथ दिया गया है। इसे गद्य और पद्य का समन्वय कहना चाहिए। प्रवचन ही नहीं संगीत भी आवश्यक है। यह इसलिए कि प्रवचन को गले उतारने पर प्रधानतया विचार क्रांति का पथ-प्रशस्त होता है। विचारों को विचारों से टकरा कर अनुपयुक्त चिन्तन छोड़ने और विवेकपूर्ण औचित्य को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। यह आवश्यक है और अनिवार्य भी, पर एक और बात है जिसे भुला नहीं दिया जाना चाहिए। वह है लोकमानस का भावनात्मक परिष्कार। विचारणा और भावना सहेलियां तो हैं, पर उनका अस्तित्व स्वतंत्र भी मानना पड़ेगा। भावना की शक्ति को समझा जाना चाहिए। वह विचारणा से भी अधिक समर्थ है। आदर्शवादी अनुगमन में तो विशुद्ध रूप से भावना की ही भूमिका रहती है। संवेदनाएं ही त्याग बलिदान की उमंगें उत्पन्न करती हैं। करुणा और सेवा का उद्गम भावना क्षेत्र के अन्तराल में ही पाया जाता है। अनास्थाजन्य प्रस्तुत संकट का निराकरण श्रद्धासिक्त उमंगें उभारने से ही बन पड़ेगा’ विचारवान प्रज्ञा इसकी प्रारम्भिक पृष्ठभूमि बनाती है। महामानवों ऋषियों, में अधिकांश भावनाशील थे। बुद्धिमान, विज्ञजन तो चतुरता के धनी ही पाये जाते हैं। वे कथनोपकथन में प्रवीण होते हैं। पर जब त्याग बलिदान का, सत्साहस के प्रकटीकरण का समय आता है तो वह बुद्धिमत्ता ही आड़े आ जाती है जिसके सहारे बड़े-बड़े प्रतिपादन खड़े किये गये थे। यह आक्षेप बहुत हद तक सही है कि बुद्धिमानों से चतुरता, प्रतिभाभर की अपेक्षा करनी चाहिए, वे आदर्शवादिता को चरितार्थ करने वाली-उदार सेना साधना से बचते कतराते ही देखे गये हैं।
यहां विचारणा का महत्व नहीं घटाया जा रहा है कि उस तक सीमित रहने, उस पर निर्भर रहने से बात बनेगी नहीं। भावना क्षेत्र को उमंगाने के लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना होगा। इसके लिए प्रतिपादनों में तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों का समावेश करके ही निश्चित नहीं हो जाना चाहिए वरन् एक कदम और आगे बढ़कर भावनाओं के भण्डार अन्तःकरण का अर्थ स्पर्श करने को महत्व देना चाहिए। हमारे प्रवचन विद्वतापूर्ण ही न हों वरन् उनके रुला देने की भी क्षमता हो। ऐसे आंसू उगाने चाहिए जो करुणा एवं उदारता बनकर सेवा साधना का क्षेत्र सम्हाल सके। आदर्शवादिता की खेती इन्हीं श्याम घटाओं से पनपती है। स्वाति बून्दों जैसा चमत्कार भाव भरी आर्द्रता ही उत्पादन कर सकती है। हमारे प्रतिपादनों में इस संवदना का समुचित समन्वय रहना चाहिए।
इस प्रसंग में एक नया तथ्य सामने आता है—संगीत की शक्ति। कहना न होगा कि जहां तक भाव संवेदना उभारने का प्रश्न है वहां तक प्रवचनों की तुलना में संगीत को कहीं अधिक-शक्तिशाली पाया गया है। सूर, मीरा, चैतन्य आदि की संगीत साधना ने अपने समय में जो चमत्कार उत्पन्न किये उन्हें भुलाया नहीं जा सकता आज भी उनकी संवेदना को जब गीतवाद्य सहित उमंगाया जाता है तो लोग लहराने लगते हैं। दीपक राग बुझे दीपक जलाते थे। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होती थी। वैसी उदाहरण अब देखने को नहीं मिलते और न इन दिनों बहेलिया हिरनों को पकड़ने के लिए वाद्य बजाकर उन्हें मंत्र मुग्ध करते हैं। सपेरे ही सांपों को लहराते देखे जाते हैं। जो हो मनुष्य के भावना क्षेत्र तक प्रवेश पाने के लिए वक्तृता से भी एक कदम आगे बढ़कर संगीत संवेदना का आश्रय लेना होगा। यही कारण है कि कथा के साथ कीर्तन शब्द को अविच्छिन्न किया गया है। गद्य के साथ पद्य का गठबंधन करने से एवं बड़ी अपूर्णता का समाधान निकलता है।
संगीत की तुलना में भावनात्मक क्षेत्र को तरंगित करने वाली शक्ति दूसरी नहीं। शास्त्रकारों ने उसकी महत्ता महिमा ‘‘शब्द ब्रह्म’’ के समतुल्य ही ‘‘नाद ब्रह्म’’ की भी गाई हैं। देवर्षि नारद की वीणा, शंकर का डमरू, कृष्ण की वंशी उनकी आन्तरिक भाव अभिव्यक्तियों का प्रकटीकरण सम्भव बनाती है। नाद योग के द्वारा मिलने वाली सिद्धियों का वर्णन यहां प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। किन्तु उस तथ्य को तो समझना ही होगा कि नव सृजन की उमंगों का उद्भव भावना क्षेत्र से होगा। और उसके लिए संगीत शक्ति को उपेक्षित नहीं रखा जा सकेगा’’ प्रवचन एवं लेखन से सामयिक आवश्यकता की पूर्ति न हो सकेगी। इस त्रिवेणी में गंगा-जमुना की लेखनी वाणी की मूर्खता भले ही रहे पर वीणापाणि सरस्वती की तीसरी धारा का समावेश भी अनिवार्य अपरिहार्य मानकर चलना होगा।
देहात के लिए संगीत की आवश्यकता एवं लोक प्रियता को प्रमुखता देनी होगी। वहां अभी भी अभिव्यक्तियों, भाषणों से नहीं गायनों से ही प्रकट की जाती है। विवाह, शादियों, तीज-त्यौहारों पर महिलाओं को गीत, मल्हार गाते सभी ने सुना है इसके अतिरिक्त आल्हा, ढोला, रामायण—नौटंकी, चौबोला, लावनी, रसिया, बाहरमासी आदि के रूप में गाये जाने वाले लोकगीतों की मंडलियां जुड़ती हैं। जो गा सकते हैं अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। शेष लोग मनोयोगपूर्वक सुनते और रात-रात भर जागते रस लेते देखे जाते हैं। लोक नृत्य समूचे भारत में सर्वत्र प्रचलित हैं। उनके अपने-अपने ढंग और स्वरूप हैं। किन्तु स्मरण रहे-वह संगीत की ही मूक अभिव्यक्ति है। गीत के साथ जो लय तरंगें उद्भूत होती हैं, वे ही कंठ ओष्ठ तक सीमित न रहकर हाथ-पैर गरदन, आंख के चल अवयवों द्वारा थिरकन बनकर फूट पड़ती है। संगीत का समूची काया तथा मनःसंस्थान को तरंगित करने वाला स्वरूप ही नृत्य माना जाता है। ‘ऐक्शन सांग’ इसी की एक मध्यवर्ती अनुकृति है। कीर्तन में पाई जाने वाली भाव-विभोर तन्मयता भी संगीत का ही विकसित एवं विस्तृत स्वरूप है।
स्वर, ताल और अंग संचालन की भाव-विभोरता कितनी मादक होती है और उसकी आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्र में क्या-क्या उपलब्धियां हस्तगत होती हैं—इसकी चर्चा विवेचना इन पंक्तियों में अभीष्ट नहीं। यहां तो इतना ही कहा जा रहा है कि नव-युग की जन-जागरण प्रक्रिया में संगीत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसकी उपयोगिता इस प्रयोजन के लिए उतनी ही है जितनी कि प्रचार पक्ष में काम आने वाले भाषण-संभाषण, लेखन-पठन, आयोजन-आन्दोलन आदि की। प्रत्येक वक्ता को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसे संगीत को साथ लेकर चलना है। प्रवचन के आदि में-अन्त में या दोनों बार संगीत सहगान या कीर्तन का समावेश रखना चाहिए। वह वाद्य यंत्रों की सहायता से बन पड़े तो आकर्षण और भी अधिक बढ़ जायेगा। अन्यथा बिना वादन का गायन भी काम दे सकता है। कथावाचक प्रायः ऐसा करते भी हैं। ‘‘हरे राम हरे कृष्ण.........।’’ ‘‘रघुपति राघव राजाराम.........।’’ ‘‘हे कृष्ण, हे कृष्ण-हरे मुरारे.........।’’ जैसी कितनी ही रामधुनें प्रख्यात हैं। आये दिन नई बनती और पुरानी विस्मृत होती रहती हैं। इन्हें एक बार वक्ता कहता है। दूसरी बार उपस्थित जन-समुदाय दुहराता है। इससे सबका ध्यान एकाग्र होता है। विश्रृंखलता, अस्त-व्यस्तता दूर होकर जागरूकता उत्पन्न होती है और कथन श्रवण का उपक्रम ठीक प्रकार चल पड़ता है।
यह परम्परा का निर्वाह हुआ। बात इतने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोक मानस में अभिनव जागरण एवं उल्लास का समावेश करने के लिए सार्थक, प्रेरणाप्रद एवं भावनाएं तरंगित करने वाले ऐसे गीतों की आवश्यकता है जो युग-चेतना को अग्रगामी बना सकें। ऐसे गीतों को ढूंढ़ने, चयन करने की आवश्यकता न पड़ेगी। उन्हें नये सिरे से लिखा जाना आरम्भ कर दिया गया है और वे बड़ी संख्या में अगले ही दिनों उपलब्ध होने लगेंगे। ‘नये सिरे से’ कहने का एक नया अभिप्राय है कि प्रज्ञा मिशन ने ‘एक ध्वनि’ को मान्यता दी है। उसमें स्वर, ताल और थिरकन इन तीनों का समावेश है। उसकी तर्ज है—
मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धापूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं।। झंकार करो ऐसी सद्भाव उभर आये। हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाये।। सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते हैं। मां तेरे चरणों में..........................।।
इसी एक ध्वनि पर असंख्यों गीत लिख जाने हैं। भिन्नताओं पर रोकथाम इसलिए लगाई गई है कि कवियों को उसी पर लिखने का अभ्यास पड़े। गायकों का गला एक ही प्रयोग पर निरन्तर अभ्यास करते-करते ठीक तरह सध जाय। वादकों के लिए इसमें सबसे अधिक सुगमता है। अनेक ध्वनियों पर वाद्य यंत्रों का अभ्यास करने के लिए स्वर शास्त्र की क्रमबद्ध शिक्षा चाहिए। अनेक सरगम में साधनी और याद करनी पड़ती हैं। स्वर ताल की भिन्नताओं को समझना और उनके अन्तर को अभ्यास में अपनाना पड़ता है, पर जब एक ही लय ध्वनि पर सारा संगीत शास्त्र समाप्त होता है तो फिर सारा झंझट ही मिटा डमरू में कुछ ही बोल निकलते हैं, शंकरजी ने उतने में ही समूह स्वर शास्त्र को केन्द्रित कर लिया तो कोई कारण नहीं कि युग संगीत को एक ध्वनि पर केन्द्रित किया जा सके। इससे गायकों को ही नहीं वादकों को भी भारी सुविधा होगी, वे इस लय का अभ्यास बिना स्वर शास्त्र की सांगोपांवा जानकारी प्राप्त किये एक से दूसरे का अनुकरण करने की विद्या अपना कर-देखते-देखते प्रवीणता प्राप्त कर सकेंगे। इशारे से ही एक साथी अपने दूसरे सहयोगी को अभ्यस्त कर दिया करेगा। कंठ से कंठ मिलाकर गाने भर से गीत क्रम पर गला सूख जाया करेगा।
वाद्य यन्त्रों में यों हारमोनियम, ढोलक, तबला अब सर्वत्र प्रचलित हैं। जहां तक एक ध्वनि का सम्बन्ध है, उन पर भी महीने दो महीने अभ्यास से काम चलाऊ ढर्रा लुढ़कने लग सकता है। महिलाएं बिना कहीं संगीत शिक्षा पाये गीत वादन का काम चलाऊ अभ्यास कर लेती हैं। फिर कोई कारण नहीं कि नियमित एक लय ताल पर सर्व साधारण को अभ्यस्त न बनाया जा सके। प्रचारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कभी पैदल कभी साइकिल पर यही है छोटे देहातों में आवश्यक सामान लेकर पहुंचने का साधन। ऐसी दशा में सफरी बाजे साथ लेकर चलने का उपाय एक ही है। कि हलके वाद्य यंत्र काम में लाये जायें। भावी प्रचार टोलियां दो-दो की होंगी और वे गांव-गांव नव युग का अलख जगाने के लिए परिभ्रमण करेंगी। उनके झोले में ही वाद्य यंत्रों को बिठाना पड़ेगा। इसलिए वे ढपली और मंजीरा-घुंघरू ही हो सकते हैं। लागत कम, वजन कम, घेरा कम, अभ्यास कम-और लाभ अधिक। इस उपाय उपचार का अवलम्बन लेकर गीत और वाद्य दोनों का समन्वय हो सकता है और वक्तृता के समतुल्य ही विचारों की अभिव्यक्ति का-जनजागरण का-एक नया द्वार खुल सकता है।
प्रत्येक युग शिल्पी को कहा गया है कि उसे अपनी वाणी मुखर करनी चाहिए और जन सम्पर्क क्षेत्र में उतर कर जन समर्थन और सहयोग उपलब्ध करने का प्रथम सोपान पूर्ण करना चाहिए। आगे की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापनाओं का द्वार इसी शुभारम्भ से खुलेगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि भाषण को ही समग्र न माना जाय वरन् उसका अविच्छिन्न सहयोगी गायन भी समान अवलम्बन बनाया जाय। वाणी के यह दोनों ही श्रृंगार हैं और अपने-अपने स्थान पर इन दोनों का ही समान उपयोग एवं महत्व है।
कथा प्रसंगों के साथ प्रवचन करने की शैली अत्यधिक सरल और सफल है। उसे शिक्षितों-अशिक्षितों में समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है और चिरकाल तक-एक ही स्थान पर नये-नये संदर्भ सुनाते रहा जा सकता है। दार्शनिक भाषणों की तरह इस प्रक्रिया को अपनाने पर तरकस कभी खाली नहीं होता और शब्द वेधी बाण निशाना बेधने के बाद फिर लौट-लौट कर तरणि को रिक्त नहीं होने देते। प्रज्ञापुराण के बीस खण्ड इसी दृष्टि से सृजे जा रहे हैं कि युग प्रवक्ताओं को अनवरत अमृत वर्षा करते हुए भण्डार चुक जाने की चिन्ता आशंका न करनी पड़े। इसी का समान्तर-सहयोगी-पूरक पथ युग गायन का है। इसे भी समान महत्व मिलना चाहिए और सीखने अपनाने में समान उत्साह रहना चाहिए।
शांति कुंज हरिद्वार में एक-एक महीने के युग शिल्पी सत्रों में भाषण और गायन के दोनों शिक्षणों की दो कक्षाएं साथ-साथ चलती हैं। जिन्हें एक महीना ठहरना है वे दोनों में से एक का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों में प्रवीणता एक साथ इतनी थोड़ी अवधि में नहीं हो सकती। जिन्हें दोनों सीखने हैं उन्हें दो महीने ठहरना पड़ेगा। इतने पर भी यह शर्त रहेगी ही कि छात्रों में इन कला कौशलों की मौलिक प्रतिभा तो रहनी ही चाहिए। जिनका संकोच हीन टूटा, उत्साह हीन उमंगा—वे भाषण कला में प्रवीणता प्राप्त न कर सकेंगे। मुंह खुलना बात दूसरी है और प्रवीणता पाना दूसरी। आजकल सर्वत्र ‘‘ए-वन’’ की मांग है इसे तो सभी जानते हैं। संगीत के बारे में भी यही बात है। गले की बनावट और ताल स्वर को समझने अपनाने की पकड़ तो अभ्यासी में होनी ही चाहिए अन्यथा अध्यापक के लाखों प्रयत्न करने पर भी आशाजनक प्रगति न हो सकेगी। फिर भी न कुछ से कुछ होना अच्छा है। शिक्षण, साधन और अभ्यास के अभाव में असंख्यों को आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। वह कठिनाई तो निश्चित रूप से इन सत्रों में सम्मिलित होने से दूर हो सकती है।
आवश्यक नहीं कि जो सीखना है, सिखाया जाना है उसके लिए हरिद्वार सत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य ही हो। यह कार्य अभ्यस्त लोग अपने साथियों को अभ्यास कराने का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर वहन कर भी पूरा कर सकते हैं। प्रशिक्षित लोग शान्ति कुंज की शैली पर अपने अपने यहां भी भाषण कला के अभ्यास की कक्षाएं चलाते रह सकते हैं और अनेकों को अभ्यस्त एवं प्रवीण बना सकते हैं। यही बात संगीत के सम्बन्ध में भी है। जिन्हें पूर्वाभ्यास है वे निर्धारित लय ध्वनि का घर बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं। नई निर्धारित ध्वनि पर बनने वाले गीतों को मंगाते सीखते और सिखाते रह सकते हैं। सुव्यवस्थित विद्यालयों में तो हारमोनियम, ढोलक, तबला भी सिखाया जा सकता है परन्तु जहां उतने साधन न हों, समय का अभाव हो, जिन्हें चलते फिरते प्रचार करना हो उनके लिए ढपली, मजीरा, घुंघरू इन दो स्वल्प व्यय साध्य, स्वल्प समय साध्य वाद्य यंत्रों को बजाना और अभ्यस्त ध्वनि मीटर का निरन्तर प्रयोग करते हुए नवीनता तथा प्रेरणा उभारते रहने का अवसर मिल सकता है।
चलते-फिरते गायन वादन में श्रोता तलाशने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। रेल में, बस में, मुसाफिर खाने में, हाट-बाजार में, धर्मशाला में, प्याऊ पर, घाट, मन्दिर, चौराहे, पार्क के आस पास कहीं भी बैठकर दो व्यक्ति मिल जुलकर ढपली, घुंघरू बजाते हुए मस्ती और प्रेरणा से भरे पूरे गीत गाने लगें तो श्रोताओं की भीड़ बिना किसी पूर्व सूचना या आमंत्रण के देखते-देखते जमा हो सकती है। इस सभा समारोह पर किसी का बंधन प्रतिबंध नहीं। जब इच्छा हुई प्रचार आयोजन आरंभ कर दिया और जब बंद करने की आवश्यकता अनुभव हुई तभी दोनों बाजे थैली में बंद किये, पल्ला झाड़ा और उठ खड़े हुए। न स्वागत की प्रतीक्षा करनी होती है और न विदाई का धन्यवाद लेने की। ढपली, घुंघरू वाला सम्मेलन समारोह ऐसा है जिसे कथा प्रवचन से भी सरल कहा जा सकता है। इसमें शक्ति का व्यय कम से कम, झंझट कम से कम तथा सरलता सुविधा अधिक से अधिक है। देहातों के लिए तो यह प्रक्रिया हर दृष्टि से सरल सफल मानी जायेगी। गीत-वाद्य के साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी व्याख्या विवेचना इतने भर से वह उद्देश्य भली प्रकार पूरा हो जाता है जिसकी पूर्ति के लिए वक्तृत्व कला सीखने सिखाने की सुव्यवस्थित योजना बनायी गयी है।
अगले दिनों साइकिलों पर तीर्थ यात्रा का, भारत भ्रमण का आन्दोलन चल पड़ेगा। युग शिल्पी बादलों की तरह खेत-खेत पर बरसने और सूखे भूखण्डों हरीतिमा लहलहाने का संकल्प लेकर निकलेंगे। गांव-गांव घर-घर, अलख जगाने की पुरातन सन्त परम्परा को पुनर्जीवन प्रदान किया जा रहा है। अपने गांव घर से हरिद्वार-हरिद्वार से दूसरे रास्ते घर पहुंचने की तीर्थ यात्रा को नये उत्साह नयी उमंगों और नयी योजनाओं के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है उसमें प्रज्ञा पुराण की कथा प्रक्रिया उतनी सफल सिद्ध न होगी जितनी कि ढपली घुंघरू के सहारे युग संगीत सुनाये और देखते-देखते श्रोताओं की भीड़ जमाकर लेने की।
कथा प्रवचन का अपना महत्व है और युग संगीत का अपना। हमें दोनों को ही महत्व देना चाहिए और आवश्यकतानुसार दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए। कथा कीर्तन की जोड़ी इसीलिए बनाई गयी है कि मुखरता के दोनों माध्यमों में अभ्यास साथ-साथ चलता रहे। अभिरुचि तथा प्रतिष्ठा को नहीं समय की मांग और लक्ष्य की पूर्ति को प्रमुखता देनी होगी।
Write Your Comments Here:
- व्यक्तित्व सम्पन्न वक्ता का प्रभावी प्रवचन
- काया की सशक्त प्रयोगशाला और शब्द शक्ति की ऊर्जा
- वाणी की शक्ति एवं प्रखरता
- वाणी में सामर्थ्य का उद्भव
- भाषण कला का आरम्भ और अभ्यास
- वक्ता को अध्ययनशील होना चाहिए
- सरल भाषण की कसौटी
- भाषण और भावाभिव्यक्ति का समन्वय
- सभा मंच पर जाने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखें
- भाषण का स्तर गिरने न दें
- आरम्भिक कठिनाई का समाधान आधी सफलता
- प्रगति इस प्रकार संभव होगी
- अभ्यास क्रम के लिए सुगम अवलम्बन
- श्रोताओं को नियमित रूप से उपलब्ध करने की सरल प्रक्रिया
- वक्ताओं को ही श्रोता भी जुटाने पड़ेंगे
- संभाषण के कुछ सारगर्भित सिद्धान्त
- मात्र भाषण ही नहीं साथ में गायन भी