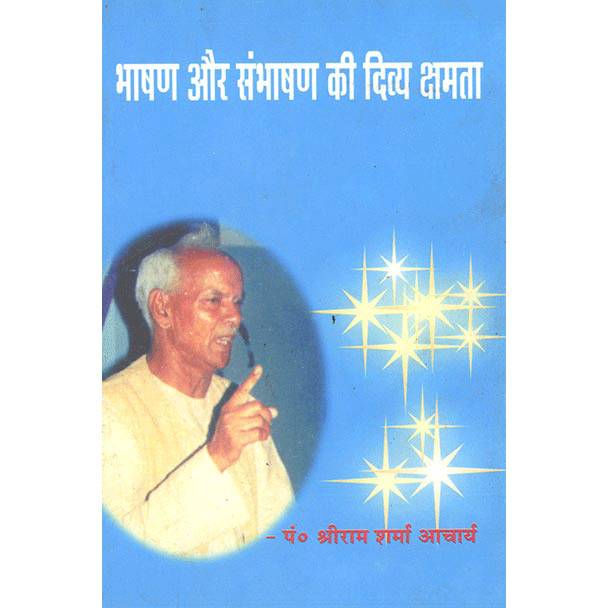भाषण और संभाषण की दिव्य क्षमता 
प्रगति इस प्रकार संभव होगी
Read Scan Version
भाषण का प्राथमिक अभ्यास करने वालों को कई कठिनाइयों का एक साथ सामना करना पड़ता है इनमें से एक है—आत्मविश्वास का अभाव। दूसरा, अधिक लोगों को एक साथ सामने उपस्थित देखकर उन्हें परीक्षक मान बैठना और उनकी दृष्टि अपने चेहरे पर लगी देखकर हड़बड़ा जाना। इन दो कारणों से वक्ता मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की चपेट में आ जाता है और जो कहना चाहिए उसकी जानकारी एवं योग्यता होते हुए भी मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाने के कारण जो कहना चाहिए था—जो कहा जा सकता था—उसे कह नहीं पाता।
कठिनाई का यह प्रथम दौर है जिसे आत्म-विश्वास जागृत करके ही सुधारा जा सकता है। अपने ऊपर विश्वास किया जाय। सोचा जाय कि जब सड़क पर बैठने वाले मदारी, रेलों में माल बेचने, नीलाम करने वाले अनपढ़-अशिक्षित वर्ग के लोग धुंआधार बोलते रह सकते हैं और उपस्थित भीड़ से तनिक भी डरते घबराते नहीं तो कोई कारण नहीं कि सुरक्षित एवं विचारशील होते हुए भी डरने घबराने की आवश्यकता पड़े। संकोचशीलता का असमंजस इस प्रकार के विचार करते रहने और साहस जगाने के लिए आत्म-प्रशिक्षण करते रहने पर यह कठिनाई आसानी से दूर की जा सकती है। एक दूसरे को प्रोत्साहन भी दें सकते हैं। कुशल वक्ता अपने अनुभव सुनाते हुए विश्वास दिला सकते हैं कि—‘‘उन्हें भी आरंभ में ऐसी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था। पर अभ्यास से प्रतीत हुआ कि वह मात्र मनोवैज्ञानिक असमंजस था। जब अभ्यास प्रारम्भ किया तो दिन-दिन यह विश्वास बढ़ता गया कि वक्तृता हर किसी के लिए सरल सुगम है। उसे अनवरत प्रयत्न करते और भूलों को ढूंढ़ते, पूछते, सुधारते क्रमशः आगे बढ़ाया जा सकता है। कुशल वक्ता के स्तर तक पहुंचा जा सकता है।’’ भूतकाल के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें आरंभ में बहुत लड़खड़ाने वाले व्यक्ति प्रयत्नरत रहकर कुशल वक्ता बने।
एकाकी प्रयास, फुरसत के समय साथियों के न रहने पर भी किये जा सकते हैं। उस समय न आत्महीनता हैरान करती है और न उपस्थिति को देख कर डरने घबराने जैसी कोई बात रहती है। इसलिए एकाकी अभ्यास में मुख्य प्रश्न एक ही रह जाता है कि विचार श्रृंखला को किस प्रकार सही रखा जाय और जो कहना है उसे बिना इधर-उधर भटके क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार व्यक्त किया जाय। विचारों में क्रमबद्धता का न होना आदि, मध्य और अन्त का पूर्व निर्धारण न रहना तीसरा व्यवधान है। इसके कारण भाषण अटपटा हो जाता है। जिस पर अधिक प्रकाश डाला जाना चाहिए उसे संक्षिप्त कर देने के उपरान्त हाथ से तीर निकल जाता है और जो छूट गया था उसे कहने में पुनरावृत्ति दोष लगता है। निर्धारित समय में अभिव्यक्ति को पूरी तरह कहने के लिए उसे कितना संक्षिप्त या विस्तृत किया जाना है—यह भाषण के पूर्व ही सोचने और निर्धारण करने का विषय है। अन्यथा या तो नियत समय से पूर्व बात समाप्त करनी पड़ेगी अथवा महत्वपूर्ण बात छूटने पर अधिक समय पाने के लिए अनुरोध करना पड़ेगा। यह दोनों ही परिस्थितियां यह प्रकट करती हैं कि भाषण की पूर्व रूप रेखा नहीं बनाई गई और जो मुंह से निकला वही कहने लगने की अस्त-व्यस्तता अपनाई गई है।
असन्तुलित विपन्नता, उत्पन्न न होने पाये—इसका एक ही उपाय है कि भाषण की आदि से अन्त तक रूप-रेखा विनिर्मित कर ली जाय और उसका कई बार अभ्यास करने के उपरान्त मंच पर जाया जाय। लेखक यही करते हैं। वे बिना सोचे समझे कलम चलाना आरंभ नहीं कर देते वरन् लिखने से पूर्व उसका ढांचा तैयार करते हैं। खाका बनाते हैं। इसके बाद रंग भरना प्रारंभ करते हैं। लेखकों को यह विचार करना पड़ता है कि आरंभ कैसे करें—मध्य में क्या-क्या तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने अभिमत की पुष्टि करें। इस ढांचे में वे गंभीरतापूर्वक सुधार परिवर्तन भी करते हैं। जब पूरी तरह विश्वस्त हो जाते हैं तब कहीं लेखन-कार्य आरम्भ करते हैं। भाषण भी एक प्रकार का लेखन ही है। सुनियोजित, लेख और सुसम्बद्ध प्रवचन की पूर्व तैयारी करना आवश्यक है। बिना पटरी बिछाये रेलगाड़ी चालू कर देने पर तो वह कहां कितनी देर में पहुंचेगी, इसका कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
महत्वपूर्ण व्यक्ति जब महत्वपूर्ण वक्तृताएं देते हैं तो उन्हें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अवसर पर बहकने न लगें, इसलिए उसे छपा लेते हैं और यथा समय पढ़कर सुना देते हैं। दीक्षान्त भाषण प्रायः इसी प्रकार छपे हुए होते हैं और संस्कार कराने वाले के द्वारा वे पढ़कर सुना दिये जाते हैं। वैज्ञानिकों की, मूर्धन्य विचारकों की, राष्ट्रसंघ के सदस्यों की महत्वपूर्ण गोष्ठियों में प्रायः हर भाषण छपा होता है ताकि समारोह समाप्त होने से पहले या बाद में उस आधार पर उपस्थित लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करने का अवसर मिल सके। यहां भाषण-कला के विद्यार्थियों को अपने भाषण छपाने और सुनाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है पर इतना तो करना ही होगा कि उसकी रूप रेखा पहले ही बना ली जाय। स्वयं न बन पड़े तो जानकारों से सलाह ले ली जाय। तैयारी के बाद उसे कई बार एकांत में दुहराना चाहिए और सांकेतिक नोट तैयार कर लेने चाहिए। यह संकेत—नोट बड़े अक्षरों में लिख लेने चाहिए। प्रवचन मंच पर सामने इस प्रकार रख लेने चाहिए कि दर्शकों यह यह बात मालूम न पड़े किन्तु स्वयं बार-बार उस पर दृष्टि डालते और एक के बाद दूसरे संकेत नोट को पूरा करते चलने की सुविधा बनी रहे।
बड़े कालेजों और विश्वविद्यालयों के व्याख्याता, दूसरे दिन जो पढ़ाना है—उसे पहले दिन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। नोट तैयार करते हैं। छात्रों के सम्मुख खड़े होकर बोलते हैं तो ‘डाइस’ पर वे नोट-कागज रखे रहते हैं। उन संकेतों पर व्याख्या चलती रहती है और अध्यापन कार्य ठीक तरह सम्पन्न हो जाता है। अध्यापक भी सन्तुष्ट रहते हैं और पढ़ने वाले छात्रों को भी उस तथ्य को पूर्ण क्रमबद्धता से सही रीति से सीख लेने की प्रसन्नता होती है। यही नीति हर वक्ता को अपनानी चाहिए। उसे अपने नोट तैयार करने चाहिए और बोलते समय उस संकेत-पट्ट को सावधानी से सामने रखना चाहिए।
‘रिहर्सल’ हर महत्वपूर्ण काम का करना चाहिए। विस्मृति भी मनुष्य की स्वाभाविक कमी है। कई दिन बीत जाने पर अभ्यस्त बातें भी दिमाग से उतर जाती हैं। इसलिए उन्हें बार-बार ‘फ्रेस’ करना पड़ता है। गायक, अभिनेता प्रायः यही करते हैं। सभा मंच पर जो गाया जाना है उसे गायक एक बार घर पर गाकर, बजाकर अपने आपको आश्वस्त कर लेते हैं।
नाटक-अभिनयों में यही होता है। नट-नर्तक आज के प्रस्तुतीकरण को रात में दिखाने से पूर्व दिन में उसका एक ‘रिहर्सल’ अवश्य कर लेते हैं। ऐसा न करें तो गायन, वादन, अभिनय में चूक हो सकती है। इतने भर से आयोजन की छवि धूमिल हो सकती है। वैसा होने देने की अपेक्षा यही अच्छा समझा जाता है कि ‘रिहर्सल’ में व्यर्थ खर्च होता दीखता समय भी आवश्यक समझा जाय और उस क्रिया को भी सम्पन्न किया जाय।
जानकार जानते हैं कि यह बात ‘पिसे को पीसने’ जैसी लगने पर भी कितनी महत्वपूर्ण-कितनी आवश्यक है। जो इसे निरर्थक समझते हैं और अहंकारवश इस संदर्भ में उपेक्षा बरतते हैं, वे घाटे में रहते हैं। ऐसे लोगों की वक्तृता में क्रमबद्धता घटती और अस्त-व्यस्तता बढ़ती रहती है भले ही वे स्वयं उस भूल को समझ, पकड़ न पायें। अच्छे लेखक भी हर लेख को दुबारा लिखते हैं। पहली बार में जो कमी रह गई थी उसे दूसरे लेखन में सुधारते, बढ़ाते निखारते हैं। अच्छे अध्यापक, लब्ध प्रतिष्ठ गायक-अभिनेताओं को भी यही करना पड़ता है। वे न अपनी पूर्णता का अहंकार करते हैं और न ‘रिहर्सल’ में अपमान जैसा कुछ अनुभव करते हैं।
इन दिनों कोई उपदेश नहीं सुनना चाहता है। पुराने जमाने की बात दूसरी थी। उन दिनों व्यास पीठ पर मात्र ऋषि कल्प व्यक्ति ही बैठने का साहस करते थे। उन्हें उपदेश देने का अधिकार भी था। लोग श्रद्धापूर्वक उन आप्त वचनों को सुनते और हृदयंगम भी करते थे। पर अब वैसी बात नहीं रही। मंच पर कोई भी जा बैठता है। गंभीर अनुभव, अध्ययन न होने पर भी—चारित्रिक विशिष्टता और विषय की पारंगतता न होने पर भी—अपना चेहरा दिखाने, आवाज सुनाने के लिए कुछ भी बकझक आरंभ कर देता। इन दिनों अनधिकारी वक्ताओं की भरमार रहती है। उनकी प्रामाणिकता पारंगतता की कोई कसौटी नहीं रही। ऐसी दशा में श्रोताओं से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे आधुनिक वक्ताओं को व्यास जी या सूतजी मानकर उनके कथन पर विश्वास करते चले जायेंगे।
इस समय परिवर्तन और अप्रमाणिकों की भरमार को देखते हुए उस तथ्य को समझना चाहिए जिसमें वक्ता का स्थान एक अच्छे वकील जितना रह गया है। उसे जनता को न्यायाधीश मानना चाहिए और निष्कर्ष निकालने, निर्णय करने का भार उसी के सुपुर्द कर देना चाहिए। वक्ता को अच्छे वकील की भूमिका निभाना चाहिए। प्रतिपाद्य विषय के पक्ष-विपक्ष में जो कुछ कहा जा सकता है उन सभी तथ्यों को जनता के सामने रखना चाहिए। यह वक्ता की कुशलता है कि विरोधी पक्ष की दलीलों को काटे, निरर्थक सिद्ध करे और अपने विषय के पक्ष में तर्क, तथ्य, प्रमाण और उदाहरणों की भरमार करता चला जाये। इस प्रकार श्रवण कर्ताओं को अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का अवसर मिलेगा और वे निर्णय को किसी के द्वारा थोपा हुआ नहीं अपने द्वारा किया गया अनुभव करेंगे।
ऐसे ही निर्णयों में गंभीरता होती है और वे सुनने वालों के गले उतर जाते हैं। इसके विपरीत यदि तर्क, तथ्य, प्रमाण आदि का प्रस्तुतीकरण न करते हुए अपनी मान्यता दूसरों पर थोपने की शैली अपनाई गई तो समझना चाहिए कि वक्ता को समय की पहचान नहीं है। वह सुनने वालों को पांच शताब्दी पूर्व के श्रद्धालु समुदाय में गिन रहा है और अपने अनुयायी मानकर उपदेश देता चला जा रहा है। अब इस शैली को अपनाने वालों पर धृष्टता करने का आक्षेप लगाया जाता है। जनता ने अपने हाथ में प्रजातंत्र संभाल लिया है। उसने एक कदम आगे बढ़कर बौद्धिक क्षेत्र में भी निर्णय निर्धारण को हथिया लिया है। अब वक्ता से इतनी ही अपेक्षा रही जाती है कि उसे जो कहना है उसके पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करके अपने कर्तव्य की इतिश्री माने।
कचहरी में वकील यही करते हैं। अदालत को अपने पक्ष में सहमत करने के लिए वे कुशलतापूर्वक तथ्य प्रस्तुत करते चले जाते हैं। वे न्यायाधीश को निर्देश नहीं करते कि अदालत यह फैसला करे। यदि कोई ऐसा करे तो उस पर अदालत के विवेक को चुनौती देने के आरोप में न्यायालय की मानहानि का अपराध ठहराया और दंडित किया जायेगा। समय की मांग है कि जनता के विवेक को मान्यता दी जाय। फैसला उसे स्वयं करने दिया जाय। वक्ता के जिम्मे अब मात्र इतना ही काम रह गया है कि उसे जो अभीष्ट है उसके पक्ष में परिपूर्ण परिश्रम करके तथ्यों को ढूंढ़ निकाले, प्रस्तुत करे और जनसमुदाय के विवेक से किसी निर्णय तक पहुंचने में सहायता भी करे। धर्म गुरु को ‘‘बास’’ की भूमिका निभाने जैसी धृष्टता इन दिनों किसी भी वक्ता के लिए शोभनीय नहीं। भले ही वह नेता विद्वान या धर्मात्मा ही क्यों न माना जाता हो। बुद्धिवाद के इस युग में सभी को अपनी रीति-नीति बदलनी पड़ रही है। वक्ताओं को भी उस परिवर्तन की आवश्यकता इच्छा या अनिच्छा से स्वीकार करनी होगी। दुराग्रह बरतने पर वे उपेक्षित-तिरस्कृत होने लगेंगे।
रटे हुए प्रवचनों से कभी काम चलता रहता था रामायण, भागवत या सत्यनारायण कथा को लोग उन्हीं रटे शब्दों में बार-बार सुनते रहते थे। यह कथा श्रवण भी पुण्य माना जाता था। पठन के बारे में भी यही बात थी, धर्म ग्रन्थों का लोग बार-बार पारायण करते रहते थे। इसे वे ‘पिसे को पीसना’ जैसा उपहासास्पद नहीं ठहराते थे और पुण्य फल समझ कर उस धर्म कृत्य को बिना ऊबे करते रहते थे। पर अब समय के साथ वह आदत भी बदल गई है। लोग नवीनता चाहते हैं। घिसी पिटी बातों में ऊब लगती है। भोजन, वस्त्र सभी कुछ नया बदलता रहना चाहिए। एक बार देखने के बाद उस फिल्म को कदाचित् ही कोई देखता हो। पोशाकों के फैशन रोज बदलते हैं। इस नवीन की पक्षधर अभिरुचि के प्रवाह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मोटर बनाने वाले हर साल नये मॉडल बदलते हैं। कलेण्डर वाले नये चित्र छापते हैं। उसी तीर्थ में हर बार पर्यटन के लिए कौन जाता है? यही बात श्रोताओं के मन में रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वे नवीनता खोजते हैं तो इसे रोका कैसे जाय? अब दो चार भाषण सीख लेने और उन्हें ही ग्रामोफोन के रिकार्डों की तरह सुनाते रहने से काम चलने वाला नहीं है। दिशा धारा भले ही निर्धारित रहे पर लहरें तरंगें तो नई-नई ही उठनी चाहिए।
नये ढंग से पुरानी बातों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि वक्ता को अध्ययनशील एवं बहुश्रुत होना चाहिए। उसे मूर्धन्य वक्ताओं के भाषण इसलिए सुनने चाहिए कि उनकी शैली में जो आकर्षक विशेषता है उसे देखा-सीखा और अपनाया जा सके। बूंद-बूंद से घड़ा भरने की बात, ज्ञान सम्पादन पर भी लागू होती है। उसके लिए नया-नया पढ़ना और नया-नया सुनना चाहिए।
वक्ता को हर विषय में चुंचु प्रवेश की अपेक्षा एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उसी मर्यादा में अपना अध्ययन संचय, अभ्यास एवं प्रतिपादन केन्द्रित कर लेना चाहिए। ऐसे ही लोग विशेषज्ञ कहलाते और अपने विषय में प्रामाणिक समझे जाते हैं। हर व्यक्ति की क्षमता सीमित है, वह थोड़े ही विषयों में विशेषज्ञ हो सकता है। सभी दिशाओं में पैर फेंकने वाले हर विषय में अपनी प्रवीणता सिद्ध करने की फिराक में रहने वाले हर विषय में अधूरे अधकचरे रह जाते हैं। ऐसी दशा में न उनकी प्रामाणिकता, विशेषता उभरती है और न जनता उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहती है। व्यक्तित्व का ऊंचा होना तो विशेष प्रयत्न और परिस्थिति पर निर्भर है पर इतना तो हर वक्ता कर सकता है कि अपने प्रतिपाद्य विषय में तथ्यों और प्रमाणों का धनी रहे और जो कहना है उसे इतने वजनदार आधार पर कहे जिससे वक्ता के अध्ययनशील की सराहना करते ही बद पड़े।
इसके लिए वक्ता का स्वाध्यायशील, बहुश्रुत एवं मनन-चिंतन में निरत विचारक भी होना चाहिए। यदि ऐसा न बन पड़ा तो फिर थोड़े से प्रसंगों पर गिनी चुनी बातें ही तोता रटंत की तरह जहां-तहां दुहराई जाती रहेंगी। नये स्थानों पर नये लोग तो उन से प्रभावित भी हो सकते हैं पर जिनने उन्हीं बातों को बार-बार दुहराते सुना है उन पर यह छाप पड़ेगी कि यहां विचारशीलता का, अध्यवसाय का अभाव है। मात्र उतना ही आता है जितना कि रट लिया गया या रटा दिया गया है। ऐसी दशा में जिन पर आरंभिक छाप पड़ी थी वह भी उस कूप मण्डूकता का पता चलने पर समाप्त हो जाती है।
दिशाधारा एक रहे तो हर्ज नहीं, पर उसके प्रतिपादन में नये तर्क-तथ्य तो प्रस्तुत किये ही जाने चाहिए उदाहरणों की कमी नहीं, घटनाएं, संस्मरण कथाएं, सूक्तियां एक ही विषय पर असंख्यों मिल सकती हैं। आवश्यकता उन्हें खोजने की है। यह खोजबीन स्वयं ही करनी पड़ती है संकलनों, उद्धरणों की कमी नहीं, पर वैसा साहित्य तो स्वयं ही ढूंढ़ना पढ़ना पड़ेगा। हर बार नया बनाना वहां तो हर हालत में अनिवार्य रूप से आवश्यक है जहां नियमित रूप से एक ही जगह परिचित लोगों के बीच अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं।
कठिनाई का यह प्रथम दौर है जिसे आत्म-विश्वास जागृत करके ही सुधारा जा सकता है। अपने ऊपर विश्वास किया जाय। सोचा जाय कि जब सड़क पर बैठने वाले मदारी, रेलों में माल बेचने, नीलाम करने वाले अनपढ़-अशिक्षित वर्ग के लोग धुंआधार बोलते रह सकते हैं और उपस्थित भीड़ से तनिक भी डरते घबराते नहीं तो कोई कारण नहीं कि सुरक्षित एवं विचारशील होते हुए भी डरने घबराने की आवश्यकता पड़े। संकोचशीलता का असमंजस इस प्रकार के विचार करते रहने और साहस जगाने के लिए आत्म-प्रशिक्षण करते रहने पर यह कठिनाई आसानी से दूर की जा सकती है। एक दूसरे को प्रोत्साहन भी दें सकते हैं। कुशल वक्ता अपने अनुभव सुनाते हुए विश्वास दिला सकते हैं कि—‘‘उन्हें भी आरंभ में ऐसी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था। पर अभ्यास से प्रतीत हुआ कि वह मात्र मनोवैज्ञानिक असमंजस था। जब अभ्यास प्रारम्भ किया तो दिन-दिन यह विश्वास बढ़ता गया कि वक्तृता हर किसी के लिए सरल सुगम है। उसे अनवरत प्रयत्न करते और भूलों को ढूंढ़ते, पूछते, सुधारते क्रमशः आगे बढ़ाया जा सकता है। कुशल वक्ता के स्तर तक पहुंचा जा सकता है।’’ भूतकाल के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें आरंभ में बहुत लड़खड़ाने वाले व्यक्ति प्रयत्नरत रहकर कुशल वक्ता बने।
एकाकी प्रयास, फुरसत के समय साथियों के न रहने पर भी किये जा सकते हैं। उस समय न आत्महीनता हैरान करती है और न उपस्थिति को देख कर डरने घबराने जैसी कोई बात रहती है। इसलिए एकाकी अभ्यास में मुख्य प्रश्न एक ही रह जाता है कि विचार श्रृंखला को किस प्रकार सही रखा जाय और जो कहना है उसे बिना इधर-उधर भटके क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार व्यक्त किया जाय। विचारों में क्रमबद्धता का न होना आदि, मध्य और अन्त का पूर्व निर्धारण न रहना तीसरा व्यवधान है। इसके कारण भाषण अटपटा हो जाता है। जिस पर अधिक प्रकाश डाला जाना चाहिए उसे संक्षिप्त कर देने के उपरान्त हाथ से तीर निकल जाता है और जो छूट गया था उसे कहने में पुनरावृत्ति दोष लगता है। निर्धारित समय में अभिव्यक्ति को पूरी तरह कहने के लिए उसे कितना संक्षिप्त या विस्तृत किया जाना है—यह भाषण के पूर्व ही सोचने और निर्धारण करने का विषय है। अन्यथा या तो नियत समय से पूर्व बात समाप्त करनी पड़ेगी अथवा महत्वपूर्ण बात छूटने पर अधिक समय पाने के लिए अनुरोध करना पड़ेगा। यह दोनों ही परिस्थितियां यह प्रकट करती हैं कि भाषण की पूर्व रूप रेखा नहीं बनाई गई और जो मुंह से निकला वही कहने लगने की अस्त-व्यस्तता अपनाई गई है।
असन्तुलित विपन्नता, उत्पन्न न होने पाये—इसका एक ही उपाय है कि भाषण की आदि से अन्त तक रूप-रेखा विनिर्मित कर ली जाय और उसका कई बार अभ्यास करने के उपरान्त मंच पर जाया जाय। लेखक यही करते हैं। वे बिना सोचे समझे कलम चलाना आरंभ नहीं कर देते वरन् लिखने से पूर्व उसका ढांचा तैयार करते हैं। खाका बनाते हैं। इसके बाद रंग भरना प्रारंभ करते हैं। लेखकों को यह विचार करना पड़ता है कि आरंभ कैसे करें—मध्य में क्या-क्या तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने अभिमत की पुष्टि करें। इस ढांचे में वे गंभीरतापूर्वक सुधार परिवर्तन भी करते हैं। जब पूरी तरह विश्वस्त हो जाते हैं तब कहीं लेखन-कार्य आरम्भ करते हैं। भाषण भी एक प्रकार का लेखन ही है। सुनियोजित, लेख और सुसम्बद्ध प्रवचन की पूर्व तैयारी करना आवश्यक है। बिना पटरी बिछाये रेलगाड़ी चालू कर देने पर तो वह कहां कितनी देर में पहुंचेगी, इसका कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
महत्वपूर्ण व्यक्ति जब महत्वपूर्ण वक्तृताएं देते हैं तो उन्हें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अवसर पर बहकने न लगें, इसलिए उसे छपा लेते हैं और यथा समय पढ़कर सुना देते हैं। दीक्षान्त भाषण प्रायः इसी प्रकार छपे हुए होते हैं और संस्कार कराने वाले के द्वारा वे पढ़कर सुना दिये जाते हैं। वैज्ञानिकों की, मूर्धन्य विचारकों की, राष्ट्रसंघ के सदस्यों की महत्वपूर्ण गोष्ठियों में प्रायः हर भाषण छपा होता है ताकि समारोह समाप्त होने से पहले या बाद में उस आधार पर उपस्थित लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करने का अवसर मिल सके। यहां भाषण-कला के विद्यार्थियों को अपने भाषण छपाने और सुनाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है पर इतना तो करना ही होगा कि उसकी रूप रेखा पहले ही बना ली जाय। स्वयं न बन पड़े तो जानकारों से सलाह ले ली जाय। तैयारी के बाद उसे कई बार एकांत में दुहराना चाहिए और सांकेतिक नोट तैयार कर लेने चाहिए। यह संकेत—नोट बड़े अक्षरों में लिख लेने चाहिए। प्रवचन मंच पर सामने इस प्रकार रख लेने चाहिए कि दर्शकों यह यह बात मालूम न पड़े किन्तु स्वयं बार-बार उस पर दृष्टि डालते और एक के बाद दूसरे संकेत नोट को पूरा करते चलने की सुविधा बनी रहे।
बड़े कालेजों और विश्वविद्यालयों के व्याख्याता, दूसरे दिन जो पढ़ाना है—उसे पहले दिन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। नोट तैयार करते हैं। छात्रों के सम्मुख खड़े होकर बोलते हैं तो ‘डाइस’ पर वे नोट-कागज रखे रहते हैं। उन संकेतों पर व्याख्या चलती रहती है और अध्यापन कार्य ठीक तरह सम्पन्न हो जाता है। अध्यापक भी सन्तुष्ट रहते हैं और पढ़ने वाले छात्रों को भी उस तथ्य को पूर्ण क्रमबद्धता से सही रीति से सीख लेने की प्रसन्नता होती है। यही नीति हर वक्ता को अपनानी चाहिए। उसे अपने नोट तैयार करने चाहिए और बोलते समय उस संकेत-पट्ट को सावधानी से सामने रखना चाहिए।
‘रिहर्सल’ हर महत्वपूर्ण काम का करना चाहिए। विस्मृति भी मनुष्य की स्वाभाविक कमी है। कई दिन बीत जाने पर अभ्यस्त बातें भी दिमाग से उतर जाती हैं। इसलिए उन्हें बार-बार ‘फ्रेस’ करना पड़ता है। गायक, अभिनेता प्रायः यही करते हैं। सभा मंच पर जो गाया जाना है उसे गायक एक बार घर पर गाकर, बजाकर अपने आपको आश्वस्त कर लेते हैं।
नाटक-अभिनयों में यही होता है। नट-नर्तक आज के प्रस्तुतीकरण को रात में दिखाने से पूर्व दिन में उसका एक ‘रिहर्सल’ अवश्य कर लेते हैं। ऐसा न करें तो गायन, वादन, अभिनय में चूक हो सकती है। इतने भर से आयोजन की छवि धूमिल हो सकती है। वैसा होने देने की अपेक्षा यही अच्छा समझा जाता है कि ‘रिहर्सल’ में व्यर्थ खर्च होता दीखता समय भी आवश्यक समझा जाय और उस क्रिया को भी सम्पन्न किया जाय।
जानकार जानते हैं कि यह बात ‘पिसे को पीसने’ जैसी लगने पर भी कितनी महत्वपूर्ण-कितनी आवश्यक है। जो इसे निरर्थक समझते हैं और अहंकारवश इस संदर्भ में उपेक्षा बरतते हैं, वे घाटे में रहते हैं। ऐसे लोगों की वक्तृता में क्रमबद्धता घटती और अस्त-व्यस्तता बढ़ती रहती है भले ही वे स्वयं उस भूल को समझ, पकड़ न पायें। अच्छे लेखक भी हर लेख को दुबारा लिखते हैं। पहली बार में जो कमी रह गई थी उसे दूसरे लेखन में सुधारते, बढ़ाते निखारते हैं। अच्छे अध्यापक, लब्ध प्रतिष्ठ गायक-अभिनेताओं को भी यही करना पड़ता है। वे न अपनी पूर्णता का अहंकार करते हैं और न ‘रिहर्सल’ में अपमान जैसा कुछ अनुभव करते हैं।
इन दिनों कोई उपदेश नहीं सुनना चाहता है। पुराने जमाने की बात दूसरी थी। उन दिनों व्यास पीठ पर मात्र ऋषि कल्प व्यक्ति ही बैठने का साहस करते थे। उन्हें उपदेश देने का अधिकार भी था। लोग श्रद्धापूर्वक उन आप्त वचनों को सुनते और हृदयंगम भी करते थे। पर अब वैसी बात नहीं रही। मंच पर कोई भी जा बैठता है। गंभीर अनुभव, अध्ययन न होने पर भी—चारित्रिक विशिष्टता और विषय की पारंगतता न होने पर भी—अपना चेहरा दिखाने, आवाज सुनाने के लिए कुछ भी बकझक आरंभ कर देता। इन दिनों अनधिकारी वक्ताओं की भरमार रहती है। उनकी प्रामाणिकता पारंगतता की कोई कसौटी नहीं रही। ऐसी दशा में श्रोताओं से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे आधुनिक वक्ताओं को व्यास जी या सूतजी मानकर उनके कथन पर विश्वास करते चले जायेंगे।
इस समय परिवर्तन और अप्रमाणिकों की भरमार को देखते हुए उस तथ्य को समझना चाहिए जिसमें वक्ता का स्थान एक अच्छे वकील जितना रह गया है। उसे जनता को न्यायाधीश मानना चाहिए और निष्कर्ष निकालने, निर्णय करने का भार उसी के सुपुर्द कर देना चाहिए। वक्ता को अच्छे वकील की भूमिका निभाना चाहिए। प्रतिपाद्य विषय के पक्ष-विपक्ष में जो कुछ कहा जा सकता है उन सभी तथ्यों को जनता के सामने रखना चाहिए। यह वक्ता की कुशलता है कि विरोधी पक्ष की दलीलों को काटे, निरर्थक सिद्ध करे और अपने विषय के पक्ष में तर्क, तथ्य, प्रमाण और उदाहरणों की भरमार करता चला जाये। इस प्रकार श्रवण कर्ताओं को अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का अवसर मिलेगा और वे निर्णय को किसी के द्वारा थोपा हुआ नहीं अपने द्वारा किया गया अनुभव करेंगे।
ऐसे ही निर्णयों में गंभीरता होती है और वे सुनने वालों के गले उतर जाते हैं। इसके विपरीत यदि तर्क, तथ्य, प्रमाण आदि का प्रस्तुतीकरण न करते हुए अपनी मान्यता दूसरों पर थोपने की शैली अपनाई गई तो समझना चाहिए कि वक्ता को समय की पहचान नहीं है। वह सुनने वालों को पांच शताब्दी पूर्व के श्रद्धालु समुदाय में गिन रहा है और अपने अनुयायी मानकर उपदेश देता चला जा रहा है। अब इस शैली को अपनाने वालों पर धृष्टता करने का आक्षेप लगाया जाता है। जनता ने अपने हाथ में प्रजातंत्र संभाल लिया है। उसने एक कदम आगे बढ़कर बौद्धिक क्षेत्र में भी निर्णय निर्धारण को हथिया लिया है। अब वक्ता से इतनी ही अपेक्षा रही जाती है कि उसे जो कहना है उसके पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करके अपने कर्तव्य की इतिश्री माने।
कचहरी में वकील यही करते हैं। अदालत को अपने पक्ष में सहमत करने के लिए वे कुशलतापूर्वक तथ्य प्रस्तुत करते चले जाते हैं। वे न्यायाधीश को निर्देश नहीं करते कि अदालत यह फैसला करे। यदि कोई ऐसा करे तो उस पर अदालत के विवेक को चुनौती देने के आरोप में न्यायालय की मानहानि का अपराध ठहराया और दंडित किया जायेगा। समय की मांग है कि जनता के विवेक को मान्यता दी जाय। फैसला उसे स्वयं करने दिया जाय। वक्ता के जिम्मे अब मात्र इतना ही काम रह गया है कि उसे जो अभीष्ट है उसके पक्ष में परिपूर्ण परिश्रम करके तथ्यों को ढूंढ़ निकाले, प्रस्तुत करे और जनसमुदाय के विवेक से किसी निर्णय तक पहुंचने में सहायता भी करे। धर्म गुरु को ‘‘बास’’ की भूमिका निभाने जैसी धृष्टता इन दिनों किसी भी वक्ता के लिए शोभनीय नहीं। भले ही वह नेता विद्वान या धर्मात्मा ही क्यों न माना जाता हो। बुद्धिवाद के इस युग में सभी को अपनी रीति-नीति बदलनी पड़ रही है। वक्ताओं को भी उस परिवर्तन की आवश्यकता इच्छा या अनिच्छा से स्वीकार करनी होगी। दुराग्रह बरतने पर वे उपेक्षित-तिरस्कृत होने लगेंगे।
रटे हुए प्रवचनों से कभी काम चलता रहता था रामायण, भागवत या सत्यनारायण कथा को लोग उन्हीं रटे शब्दों में बार-बार सुनते रहते थे। यह कथा श्रवण भी पुण्य माना जाता था। पठन के बारे में भी यही बात थी, धर्म ग्रन्थों का लोग बार-बार पारायण करते रहते थे। इसे वे ‘पिसे को पीसना’ जैसा उपहासास्पद नहीं ठहराते थे और पुण्य फल समझ कर उस धर्म कृत्य को बिना ऊबे करते रहते थे। पर अब समय के साथ वह आदत भी बदल गई है। लोग नवीनता चाहते हैं। घिसी पिटी बातों में ऊब लगती है। भोजन, वस्त्र सभी कुछ नया बदलता रहना चाहिए। एक बार देखने के बाद उस फिल्म को कदाचित् ही कोई देखता हो। पोशाकों के फैशन रोज बदलते हैं। इस नवीन की पक्षधर अभिरुचि के प्रवाह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मोटर बनाने वाले हर साल नये मॉडल बदलते हैं। कलेण्डर वाले नये चित्र छापते हैं। उसी तीर्थ में हर बार पर्यटन के लिए कौन जाता है? यही बात श्रोताओं के मन में रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वे नवीनता खोजते हैं तो इसे रोका कैसे जाय? अब दो चार भाषण सीख लेने और उन्हें ही ग्रामोफोन के रिकार्डों की तरह सुनाते रहने से काम चलने वाला नहीं है। दिशा धारा भले ही निर्धारित रहे पर लहरें तरंगें तो नई-नई ही उठनी चाहिए।
नये ढंग से पुरानी बातों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि वक्ता को अध्ययनशील एवं बहुश्रुत होना चाहिए। उसे मूर्धन्य वक्ताओं के भाषण इसलिए सुनने चाहिए कि उनकी शैली में जो आकर्षक विशेषता है उसे देखा-सीखा और अपनाया जा सके। बूंद-बूंद से घड़ा भरने की बात, ज्ञान सम्पादन पर भी लागू होती है। उसके लिए नया-नया पढ़ना और नया-नया सुनना चाहिए।
वक्ता को हर विषय में चुंचु प्रवेश की अपेक्षा एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उसी मर्यादा में अपना अध्ययन संचय, अभ्यास एवं प्रतिपादन केन्द्रित कर लेना चाहिए। ऐसे ही लोग विशेषज्ञ कहलाते और अपने विषय में प्रामाणिक समझे जाते हैं। हर व्यक्ति की क्षमता सीमित है, वह थोड़े ही विषयों में विशेषज्ञ हो सकता है। सभी दिशाओं में पैर फेंकने वाले हर विषय में अपनी प्रवीणता सिद्ध करने की फिराक में रहने वाले हर विषय में अधूरे अधकचरे रह जाते हैं। ऐसी दशा में न उनकी प्रामाणिकता, विशेषता उभरती है और न जनता उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहती है। व्यक्तित्व का ऊंचा होना तो विशेष प्रयत्न और परिस्थिति पर निर्भर है पर इतना तो हर वक्ता कर सकता है कि अपने प्रतिपाद्य विषय में तथ्यों और प्रमाणों का धनी रहे और जो कहना है उसे इतने वजनदार आधार पर कहे जिससे वक्ता के अध्ययनशील की सराहना करते ही बद पड़े।
इसके लिए वक्ता का स्वाध्यायशील, बहुश्रुत एवं मनन-चिंतन में निरत विचारक भी होना चाहिए। यदि ऐसा न बन पड़ा तो फिर थोड़े से प्रसंगों पर गिनी चुनी बातें ही तोता रटंत की तरह जहां-तहां दुहराई जाती रहेंगी। नये स्थानों पर नये लोग तो उन से प्रभावित भी हो सकते हैं पर जिनने उन्हीं बातों को बार-बार दुहराते सुना है उन पर यह छाप पड़ेगी कि यहां विचारशीलता का, अध्यवसाय का अभाव है। मात्र उतना ही आता है जितना कि रट लिया गया या रटा दिया गया है। ऐसी दशा में जिन पर आरंभिक छाप पड़ी थी वह भी उस कूप मण्डूकता का पता चलने पर समाप्त हो जाती है।
दिशाधारा एक रहे तो हर्ज नहीं, पर उसके प्रतिपादन में नये तर्क-तथ्य तो प्रस्तुत किये ही जाने चाहिए उदाहरणों की कमी नहीं, घटनाएं, संस्मरण कथाएं, सूक्तियां एक ही विषय पर असंख्यों मिल सकती हैं। आवश्यकता उन्हें खोजने की है। यह खोजबीन स्वयं ही करनी पड़ती है संकलनों, उद्धरणों की कमी नहीं, पर वैसा साहित्य तो स्वयं ही ढूंढ़ना पढ़ना पड़ेगा। हर बार नया बनाना वहां तो हर हालत में अनिवार्य रूप से आवश्यक है जहां नियमित रूप से एक ही जगह परिचित लोगों के बीच अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं।
Write Your Comments Here:
- व्यक्तित्व सम्पन्न वक्ता का प्रभावी प्रवचन
- काया की सशक्त प्रयोगशाला और शब्द शक्ति की ऊर्जा
- वाणी की शक्ति एवं प्रखरता
- वाणी में सामर्थ्य का उद्भव
- भाषण कला का आरम्भ और अभ्यास
- वक्ता को अध्ययनशील होना चाहिए
- सरल भाषण की कसौटी
- भाषण और भावाभिव्यक्ति का समन्वय
- सभा मंच पर जाने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखें
- भाषण का स्तर गिरने न दें
- आरम्भिक कठिनाई का समाधान आधी सफलता
- प्रगति इस प्रकार संभव होगी
- अभ्यास क्रम के लिए सुगम अवलम्बन
- श्रोताओं को नियमित रूप से उपलब्ध करने की सरल प्रक्रिया
- वक्ताओं को ही श्रोता भी जुटाने पड़ेंगे
- संभाषण के कुछ सारगर्भित सिद्धान्त
- मात्र भाषण ही नहीं साथ में गायन भी