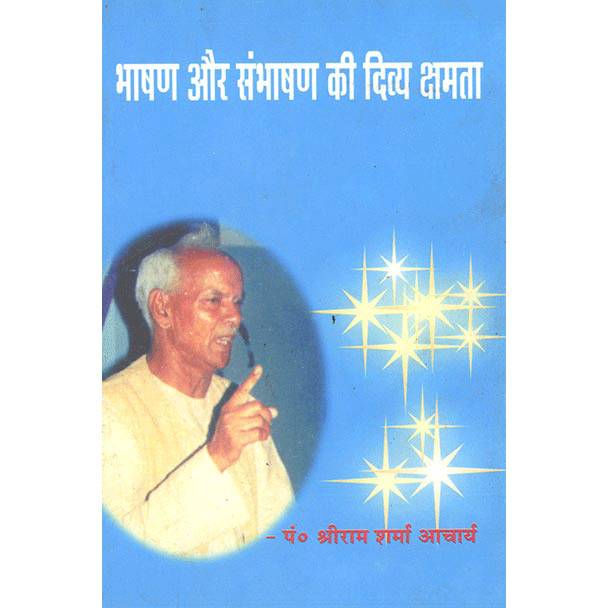भाषण और संभाषण की दिव्य क्षमता 
वक्ताओं को ही श्रोता भी जुटाने पड़ेंगे
Read Scan Version
शास्त्रकारों ने वाणी को सरस्वती और वक्ता को मुनि, मनीषी, ऋषि कहा है। दूसरों की विचारणा और भावना उभारने वाले, जीवन प्रवाह को दिशा देने वाले, वातावरण को मोड़ने वाले निश्चित रूप से विशिष्ट शक्ति सम्पन्न कहे जायेंगे यह समर्थता वक्ता के निज के लिए अनेकों सफलताएं उत्पन्न करती हैं, प्रगति के अनेकों द्वार खोलती हैं और साधारण को असाधारण स्तर तक उछाल देती हैं। लोक मंगल की दृष्टि से यह सर्वोच्च स्तर का परमार्थ, सत्परामर्श एवं प्रेरणा-अनुदान के माध्यम से ही बन पड़ता है। इस सामर्थ्य का समग्र विकास करने एवं उसका सदुपयोग करने से असंख्यों महामानव स्वयं कृत-कृत्य हुए और दूसरों के लिए दैवी वरदान जैसी सहायता कर सकने वालों में गिने गये। बुद्ध, तिलक, महावीर, गांधी, विवेकानन्द, दयानन्द आदि असंख्यों लोक नायकों ने जिस माध्यम से समय की महती सेवा सम्पन्न की उसमें उनकी वाक् शक्ति का चमत्कार अविस्मरणीय ही माना जायगा।
वाक् सिद्धि के लिए व्यक्तित्व में भावनात्मक उत्कृष्टता का समावेश करना होता है। साथ ही स्वभाव-व्यवहार में सज्जनोचित शालीनता का गहरा पुट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आत्म संयम और उदार व्यवहार की उभयपक्षीय साधना में चिरकाल तक निरत रहना पड़ता है।
कहा जा चुका है कि वाणी एक शक्ति भी है और एक कला भी। शक्ति तब बनती है जब उसके साथ वक्ता के चिन्तन, चरित्र और व्यवहार की उत्कृष्टता जुड़ गयी हो। कला तब कहलाती है जब बोलने का लहजा, करीना, तरीका, प्रवाह ठीक तरह चलाने का अभ्यास कर लिया जाय। शक्ति और कला का समन्वय होने से चमत्कारी परिस्थितियां सामने आती हैं। मुखर न हो सकने वाली ऋषि वाणी भी अपंग है और मात्र नाटकीय वाचालता सीखी गई हो तो उससे मंच के अभिनेताओं द्वारा कौतुक-कौतूहल उत्पन्न हो सकता है।
युगशिल्पियों की वाक्शक्ति को वाक् सिद्धि स्तर तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए वाणी का संयम अपनाना चाहिए। सामान्य बोलचाल में सचाई, नम्रता, हितकामना का समावेश करते रहा चाहिए। आत्मश्लाघा, क्रोध, विद्वेष, छल, प्रपंच का समावेश रहने पर वाणी अपनी प्रभाव शक्ति खो बैठती है। इसी प्रकार अभक्ष्य खाने वाली जिह्वा भी दग्ध, अपंग स्तर की बन जाती है और विनोद से बढ़कर और कोई गंभीर प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। सरस्वती की साधना यही है कि वाणी का उच्चस्तरीय उपयोग होता रहे। उसे न कहने योग्य न कहने दिया जाय, न खाने योग्य न खाने दिया जाय। इतना बन पड़े तो वाणी के शक्ति रूप में प्रकट होने की संभावना बन गई। शब्द को बाण और व्यक्तित्व को धनुष कहा गया है। दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही निशाना सधता है। यह तथ्य ध्यान में बना रहे तो क्रमशः जीवनक्रम में अधिकाधिक पवित्रता एवं प्रखरता का समावेश करने वाली आत्मसाधना चलेगी और वक्ता की वाणी मंत्र बोलने लगेगी। मंत्र उच्चस्तरीय विचारणा से प्रेरित संभाषण को कहते हैं। मन्त्र की शक्ति सर्वविदित है। मन्त्र सिद्धि और वाक् सिद्धि एक ही तथ्य के दो नाम हैं।
युग सन्धि की वेला में प्रज्ञा-परिजनों को प्रस्तुत महाभारत में अपने अस्त्र-शस्त्र सजाने चाहिए। इसमें सत्परामर्श को ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयुक्त करने की कुशलता इन्हीं दिनों सीखनी चाहिए। सीखने के लिए साधन चाहिए और वातावरण भी। पहलवान बनने के लिए व्यायामशाला, विद्वान बनने के लिए पाठशाला, धनी बनने के लिए उद्योगशाला का आश्रय लिये बिना गति गति नहीं। तैरना सीखने वालों को तालाब में प्रवेश करना होता है। भोजन पकाने के लिए आवश्यक उपकरणों वाला रसोईघर चाहिए। साधनों के अभाव में गायन, वादन, चित्र, प्रतिमा, शिल्प, चिकित्सा आदि किसी भी योग्यता का प्रमाण-परिचय दे सकना संभव नहीं होता। इसलिए वाक् सिद्धि के लिए जहां वक्ता को अपने व्यक्तित्व को, विशेषतया वाणी को संयम-साधना की कसौटी पर खरा सिद्ध करना होता है, वहीं उसकी कला में सौंदर्य, माधुर्य भर देने का अभ्यास भी आवश्यक है। हीरा खरादा जाता है, सोना गलाया जाता है तभी उनकी विशिष्टता निखरती है। आभूषण बनने की स्थिति तक उन्हें अनेक बार—अनेक प्रकार से संस्कारित किया जाता है। वाणी को सुसंस्कारी बनाने का प्रयास भी इसी प्रकार होना चाहिए।
अभ्यास की अपनी आवश्यकता है। कला के रूप में वाणी को परिष्कृत करने के लिए तदनुरूप अवसर चाहिए। इसके लिए श्रोताओं की उपस्थिति एवं मनःस्थिति में उर्वरता होनी चाहिए, अन्यथा बोया गया बीज ऐसे ही सड़ेगा-घुनेगा और चिड़ियों के पेट में चला जायगा। उसे अंकुरित-पल्लवित होने का अवसर ही न मिलेगा। ऐसे श्रोता भी हमें अपने ही प्रयत्न से जमा करने होंगे। दूसरों द्वारा एकत्रित की गई भीड़ उन्हीं के स्तर तथा रुझान की होगी जैसी कि संयोजकों की है। अपने प्रयोग अभ्यास के लिए हमें अपने ही स्तर का जन-समुदाय एकत्रित करना चाहिए और उस एकत्रीकरण में भी दूसरों का मुंह ताकने की अपेक्षा स्वयं ही पराक्रम-पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरे भीड़ जुटायें, मंच बनायें और उस पर अपने से जा विराजने का अनुरोध करें। इस आशा में बैठे रहने पर कदाचित् ही वैसा अवसर कभी मिलेगा; क्योंकि आयोजन कभी-कभी ही किन्हीं के प्रयत्न से बहुत समय बाद सम्पन्न होते हैं। उनमें भी यह विश्वास नहीं कि अपने को बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं। ऐसी दशा में उचित यही है कि जितनी उत्कंठा अपनी बात लोगों को सुनाने; गले उतारने की है उतनी ही चेष्टा आयोजन के सूत्र संचालन के निमित्त की जाय। युग-शिल्पियों को न केवल वक्ता वरन् समुदाय को एकत्रित कर सकने में समर्थ संयोजक भी होना चाहिए।
प्रज्ञा अभियान के अन्तर्गत वर्ष में कई बार कई स्थानीय आयोजन करने के लिए कहा गया है। इन्हें पर्व आयोजन कहा गया है। वसन्त पंचमी, होली, गायत्री जयन्ती, गुरुपूर्णिमा, श्रावणी, दिवाली ऐसे ही पर्व हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मनाया जाना चाहिए। इन आयोजनों के साथ व्यक्ति, परिवार और समाज की उच्चस्तरीय संरचना में भारी योगदान देने वाली प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि उन्हें सामूहिक रूप से मनाया जाय और उस तथ्य का स्मरण दिलाया जाय जिनमें शालीनता बनाये रहने और सत्प्रयत्नों के लिए पराक्रम करने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए किस प्रक्रिया को किस प्रकार अपनाया जाय। इस विस्मृत पक्ष को इन दिनों विशेष रूप से उभारा जाना चाहिए। प्रयत्न यह होना चाहिए कि पर्व मनाने की सामूहिक विधि-व्यवस्था को नये सिरे से पुण्य परम्परा का एक रूप दिया और उसमें सम्मिलित रहने के लिए सर्वजनीन उत्साह उत्पन्न किया जाय।
युग सृजन के प्रवक्ताओं को वाक् शक्ति का व्यापक उपयोग करने के लिए मात्र कथन की एकांगी कार्यपद्धति अपनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें दो मोर्चों पर दुधारी तलवार लेकर जूझना पड़ेगा। एक कार्य यह कि वे वाणी के कलाकार बनें और उसे प्रभावी बनाने के लिए अपने चरित्र-चिन्तन को उच्चस्तरीय बनावें। दूसरा यह कि श्रवणकर्त्ताओं को जुटायें। उनमें इस प्रकार की अभिरुचि उत्पन्न करें। यह दोनों ही कार्य सम्पन्न कर सकने वाले ही कुशल वक्ता की भूमिका निभा सकेंगे। जो इन दो प्रसंगों के साथ जुड़े हुए दो-दो कार्यक्रमों में से एक को भी महत्वहीन समझेंगे, एक की भी उपेक्षा करेंगे वे वाचाल भले ही कहला सकें, नव-युग के प्रवक्ता नहीं कहे जा सकेंगे। हमें एकांगी प्रयास से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वरन् समग्र प्रयास का संयोजक होना चाहिए।
वाणी में शक्ति उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसमें कलाकारिता का समावेश कैसे हो सकता है—इस पर पिछली पंक्तियों में सैद्धान्तिक प्रकाश डाला जा चुका है; उसका व्यवहार तो हर व्यक्ति को अपनी मनःस्थिति और परिस्थिति देखते हुए स्वयं ही निर्धारित करना होगा। किसके चरित्र-चिन्तन में क्या कमी है और उसे सुधारने के लिए किन परिस्थितियों में किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है—इसका निर्धारण अन्य व्यक्ति कदाचित ही कर सकें। कुछ सहायक वे हो सकते हैं जो साथ रहते हैं और स्थिति के साथ तालमेल बिठाने वाला परामर्श दे सकते हैं। हर वक्ता को विचारशील होना चाहिए। जन मानस को—लोक प्रवाह को सुधारने की जिम्मेदारी उठाने वालों में इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व को इस ढांचे में ढालें कि वे सच्चे अर्थों में सरस्वती के उपासक, वाक्शक्ति के धनी और लोक मानस को उलट सकने में समर्थ सिद्ध हो सकें। बड़े वरदान पाने के लिए बड़ा तप करना चाहिए। यह साधना का विषय है, उसमें धैर्य और संकल्प का समान रूप से प्रयोग करना पड़ेगा और बन्दर वृत्ति जैसी चंचलता को एक कोने पर रखकर एकाग्र-एकनिष्ठ बनने के लिए प्रयत्नरत होना पड़ेगा। यह एक पक्ष ऐसा है जो एकांकी संयोजन और प्रयत्न के आधार पर स्वयं ही सम्पन्न किया जा सकता है; दूसरों के सहयोग की इसमें नगण्य-सी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा प्रयास थोड़ा कठिन है। उसमें न दूसरों से सम्पर्क साधने की, उन्हें सहमत करने, सहयोगी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। श्रोता जुटाना बड़ा काम है। दूसरे क्यों किसी की मर्जी पर चलें? क्यों अपना समय किसी की इच्छापूर्ति के लिए दें? विशेषतया तब, जबकि अपनी योग्यता उतनी नहीं उठ सकी कि श्रोता बहुत कुछ पाने की आशा से एकत्रित हों और बहुत दिनों तक- बहुत समय तक उसके लिए आते रहें। अभ्यास में प्रवीणता एक दिन में तो आती नहीं। उसके लिए सहयोगी श्रोता न जुट सकें तो समझना चाहिए कि गाड़ी का एक पहिया टूट गया। उड़ने के लिए आवश्यक दो पंखों में से एक कट गया। एक हाथ से ताली कैसे बजेगी?
चूहा अपना बिल स्वयं खोदता है पर सांप बने बिल में घुस पड़ने की घात लगाता है। हमें सांप नहीं चूहा बनना चाहिए। दूसरों के आयोजित सम्मेलनों की ताक में रहने और जित-तिस के द्वारा बनाये मंचों पर जो विराजने वाली ललक है वह है तो सरल और सुनहरी, पर उसे व्यावहारिक नहीं मानना चाहिए। जिनने अपने मंच बनाये, सम्मेलन बुलाये हैं, वे उपस्थिति को प्रसन्न करने वाले वक्ता बुलाते हैं। जिनसे पैसा लिया है, जिनने समय दिया है उनकी मर्जी पूरी न करने पर आगे का रास्ता बन्द होता है। इसलिए विभिन्न संयोजक सदा मूर्धन्यों को बुलाते हैं और नौ सिखियों का पत्ता काटते हैं। फिर वे यह भी देखते हैं वक्ता लोकरुचि के अनुरूप बोलने का अभ्यस्त है या नहीं। अपना मिशन लोकरुचि से विपरीत न सही भिन्न तो है ही। ऐसी दशा में लोकरुचि को प्रधानता देने वाले संयोजक उसी प्रकार की व्यवस्था बनाते और वैसे ही वक्ता बुलाते हैं। हमें अपना ही कुआं खोदना और अपने हाथ से खींचा पानी पीने की तैयारी करनी चाहिए।
जिन दिनों चाय का प्रचलन नहीं था, उन दिनों उसके प्रचारक घर-घर जाते थे। हाथों में गरम चाय की बन्द बाल्टी और गिलास कुल्हड़ होते थे। सवेरा होते-होते घरों पर पहुंचते, दरवाजे खटखटाते, आवाज लगाते थे—गरम चाय पीने की। ‘‘चाय पियो-बहुत दिन जियो’’का नारा लगाते थे और जो थोड़ी भी रुचि लेता था उसे मुफ्त चाय पिलाते थे। जो अच्छी लगने की बात कहता उससे एक पैसे वाला चाय का पैकेट खरीदने का अनुरोध करते। बनाने की विधि सिखाते और कहते इस एक पैकिट में चार कप उम्दा चाय घर पर बन सकती है। उसे पीने से क्या-क्या लाभ होते हैं यह बताने का वे तब तक क्रम जारी रखते थे जब तक कि सहमति सूचक सिर न हिलने लगता। इन चाय प्रचारकों के स्टॉल हाट-बाजारों में पहुंचते और उधर घूमने-फिरने वाली भीड़ को आकर्षित करके वही उपक्रम चलाते जो आये दिन घर-घर जाकर करना पड़ता। यह जन सम्पर्क ही था जिसके कारण चाय अन्न-वस्त्र की तरह अपना स्थान अनिवार्य दैनिक आवश्यकताओं में बना लिया है। भोर होने से पहले और बहुत रात बीते तक स्टालों पर भीड़ लगी रहती है।
युगान्तरीय-चेतना के प्रति वर्तमान स्थिति में उपेक्षा स्वाभाविक है। हर अजनबी सुधारवादी प्रस्तुतीकरण का प्रारंभ में उपहास-तिरस्कार होता रहा है। बहुत दिन बाद ही सतत प्रयास से प्रवाह को मोड़ना सम्भव हुआ है। यही बात वर्तमान लोक मानस के सम्बन्ध में भी है। उससे अपरिचित तथ्यों से परिचित कराने से लेकर सहमत बनाने तक की लम्बी मंजिल युग-शिल्पियों को ही पूरी करनी पड़ेगी। वक्तृता का उपयोग सही लोगों में सही स्तर पर हो सके, इसके लिए चाय प्रचारकों की नीति अपनानी पड़ेगी। उस लम्बी भूमिका के निर्वाह में जितनी प्रगति होगी उतना ही सफलता का पथ प्रशस्त होगा।
प्रज्ञा अभियान के आरंभिक दो प्रयोगों में से एक है घर-घर हर शिक्षित को नियमित रूप से प्रज्ञा साहित्य पढ़ाने और वापिस लेने के लिए जाना। ज्ञान रथ इसी के लिए जगह-जगह बनाये और चलाये जा रहे हैं। दूसरा प्रयोग है स्लाइड प्रोजेक्टर। मोहल्ले-मोहल्ले प्रकाश चित्रों को दिखाते हुये युगान्तरीय चेतना का आलोक जन-जन के मन-मन में प्रवेश करना। इसमें लोकरंजन और लोक मंगल दोनों का समन्वय होता है और जनता को एकत्रित करने में कहीं भी कठिनाई नहीं पड़ती। मुहल्ले के बाल-वृद्ध, नर-नारी सहज ही उस विनोद कौतूहल को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। इन दोनों प्रयोगों में वक्तृत्व कला के अभ्यासी को भाषण और संभाषण दोनों का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। घर-घर साहित्य देने वापिस लेने के लिए जाने पर कुछ तो पूछना बताना ही पड़ेगा। पोस्टमैन की तरह तार चिट्ठी फैलाकर तो चल नहीं देना है। अपना प्रयोजन और पुस्तकों का माहात्म्य बताये बिना तो पढ़ने वालों की अभिरुचि ही नहीं जगेगी। साहित्य प्रसार की प्रक्रिया में संभाषण कला का अभ्यास करने और उसे विकसित और परिष्कृत करने की पूरी-पूरी गुंजाइश है। जन सम्पर्क साधने से ही समर्थन और सहयोग प्राप्त करने की सफलताओं का दर्शन हो सकेगा। सम्पर्क साधने में प्रज्ञा-साहित्य का प्रचार सर्वोत्तम है। इसमें देना ही देना है लेना कुछ नहीं। ऐसी प्रक्रिया लोकप्रिय क्या न होगी? इसमें निरत लोगों को सहानुभूति क्यों नहीं मिलेगी? कृतज्ञता का लाभ निश्चित रूप से लौट कर मिलेगा।
इसी प्रकार दूसरे प्रयोग ‘स्लाइड प्रोजैक्टर’ में भाषण कला का अभ्यास अनवरत रूप से चलता रहा सकता है। आज इस मुहल्ले तो कल उस मुहल्ले की योजना बना लेने पर पूरे वर्ष यह कार्यक्रम चलता रह सकता है। एक वर्ष की स्लाइडें जब तक पूरी होती हैं तब तक नये वर्ष के अगले चित्र बन कर आ जाते हैं और यह चलता फिरता सिनेमा, नई-नई फिल्म स्लाइडें दिखाते हुये अपनी प्रचार प्रक्रिया का निश्चित रूप से गतिशील रखे रह सकता है। भाषण-कला के अभ्यास में जनता को एक एकत्रित करने का इससे सरल, सस्ता, आकर्षक और सुनियोजित तरीका और कोई हो ही नहीं सकता।
यह चलती फिरती प्रक्रिया हुई। इससे आगे का सभा—सम्मेलनों का—विचार गोष्ठियों का वह स्वरूप बनता है जिसमें मंच से बोलने की प्रक्रिया सधती है। इसमें जन्मदिवसोत्सव मनाने की बात पहले कही जा चुकी है। इस स्तर के आयोजन अपनी मित्र मंडली से आरंभ किये जा सकते हैं और किसी को भी प्रोत्साहित करके, इस हर्षोत्सव के लिए बात की बात में सहमत किया जा सकता है। दो चार रुपये खर्च करने जैसी छोटी सी व्यय व्यवस्था निर्धन से निर्धन भी वहन कर सकता है विशेषतया तब, जब उसे हीरो बनने का अवसर मिलता है, और घर पर मित्र सम्बन्धियों को एकत्रित होने का आनन्द मिलता है। आतिथ्य खर्चीला न होने पाये, इस प्रतिबन्ध से यह कार्यक्रम नितान्त सरल हो गये हैं। हवन की प्रक्रिया इतनी सरल सस्ती बना दी गयी है कि वह एक दो रुपये में ही अच्छा खासा वातावरण बनाने और उत्साह उत्पन्न करने की आवश्यकता पूरी करती है। यदि अपना निश्चय हो तो सप्ताह में एक आयोजन का प्रबंध अपने एकाकी प्रयत्न से- अपने ही सम्पर्क क्षेत्र में भली प्रकार हो सकता है। वक्तृता के लिए मंच तैयार मिल गया न? महिलाएं यह कार्य महिलाओं का जन्म दिन मनाकर—बच्चों के षोडश संस्कारों की योजना बना कर अपने क्षेत्र में मूर्धन्य बन सकती हैं और वक्तृता के अभ्यास में निपुण हो सकती हैं।
पर्व आयोजन इससे बड़ी और अधिक प्रभावी योजना है। वसन्त, होली, गायत्री जयंती (गंगा दशहरा), गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, सिद्ध अमावस्या, दीवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि पर्वों की छुट्टियां होती ही हैं। लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर इन प्रयोजनों के पीछे उद्देश्य क्या है। इन पर्वों पर रात्रि को या प्रातः काल जब स्थानीय सुविधा दीखे, एक छोटा पर्व आयोजन किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा धार्मिक कर्मकाण्ड मिला रहने से वातावरण में श्रद्धा का पुट लगता है। और साथ ही लोक शिक्षण की विभिन्न दिशा धाराओं पर प्रकाश डालने का इन पर्वों पर सहज अवसर मिलता है। इन आयोजनों के लिए वक्तृत्व कला के अभ्यासी को स्वयं भी प्रयत्नरत रहना चाहिए और साथी सहयोगियों की सहायता से उसे आकर्षक, सफल बनाने में जुटना चाहिए। यह प्रवाह उलटने की दृष्टि से तो महत्व पूर्ण है ही, अभ्यासी को अपने लिए स्वनिर्मित मंच खड़ा करने और अभ्यास बढ़ाने का भी सुयोग सहज ही मिलता है। बड़े सम्मेलनों में बड़े वक्ता की तलाश होती है पर जन्म दिवसोत्सव और पर्वों की मुहल्ला गोष्ठियों में तो आरम्भिक वक्ता भी मान-सम्मान पाता है।
दूसरे बड़े आयोजन नवरात्रियों के साधना पर्व हैं। इन नौ दिन लगातार चलने वाले सामूहिक धर्मानुष्ठान आयोजनों में जो भागीदार बनते हैं, नियमित रूप से उपस्थिति होते ही हैं। साथ ही पांच अन्य साथियों को घसीट कर लाने की बात भी उनकी पुण्य प्रक्रिया में सम्मिलित की गयी है। इस आधार पर बसी अनुष्ठान कर्ता अपने साथ सौ और समेट लाते हैं। कुछ इधर उधर के आ जाने से डेढ़ दो सौ की उपस्थिति पूरे नौ दिन तक बनी रहती है। वर्ष में दो बार यह अवसर आते हैं। गायत्री के माध्यम से प्रज्ञा अभियान के समस्त प्रतिपादनों को उपस्थित समुदाय को हृदयंगम कराने में सुविधा होती है। ऋतम्भरा गायत्री की साधना और प्रज्ञा-अभियान की युगान्तरीय चेतना एक ही तथ्य के दो रूप हैं। दोनों का समन्वय बड़ी सरलता और सुन्दरता के साथ निभ जाता है। नव रात्रि सत्रों के अन्यान्य अनेकों लाभ है। उनमें से एक लाभ यह भी है कि वक्तृत्व कला के अभ्यासी स्थानीय आयोजनों में विचार व्यक्त करते-करते इतने अभ्यस्त निपुण बन सकते हैं कि बृहत् सम्मेलनों में प्रमुख वक्ता की आवश्यकता पूर्ण कर सकने में सफल हो सकें।
जहां बोलने में अड़चन पड़ती हो विचारों का तारतम्य न बैठता हो वहां पढ़कर सुना देना भी एक उपाय है। युग साहित्य जिन हाथों से लिखा जा रहा है उसमें जो आग रहती है उसकी समीपता तथा गर्मी सभी को रुचती है। यह कहा जाय कि एक प्रेरणा स्रोत के अन्तराल से निकली ऊर्जा को उपस्थित लोगों तक पहुंचाने, उससे अवगत कराने भर का विनम्र प्रयास किया जा रहा है तो उपस्थित लोग किसी लेख को सुनने के लिये भी उतने ही उत्साह से तैयार रहते हैं कितना कि स्थानीय वक्ता का भाषण सुनने के लिए। छपे को पढ़कर सुना देने में भी कलात्मक उभार लाने पड़ते हैं। इस भाव अभिनय के लिए इस प्रकार सुनाये जाने वाले भाषणों में अधिक गुंजाइश रहती है। क्योंकि इनमें कुछ सोचने याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही प्रवाह क्रम बिगड़ने जैसी अड़चन भी सामने नहीं आती। ज्ञान गोष्ठियों में इस प्रकार लेख या पुस्तकों का अंश सुना देने का भी कम से कम प्रज्ञा परिजनों को तो अवसर है ही। वे इसे सुनने में जिस हस्ती का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे उस वक्तृता में भागीदार रखने से जहां अपना वजन हल्का होता है वहां भी उसकी प्रभावशक्ति में कोई कमी नहीं आती।
वक्तृता के अभ्यास के लिए दूसरा चरण यही है कि अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति हो और सुनने और समझने के लिए पूर्व भूमिका ऐसी हो जिसमें सुनने वालों को अपनी मर्जी के विपरीत सुनने पर अनख न लगे, अरुचि उत्पन्न न हो और बीच में ही उठ चलने जैसी कुरुचिपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न न हो। इस उपचार को जो भी अपनायेंगे उसे भाषण शिक्षा का एक अनिवार्य अंग मानेंगे और अपने श्रोता आप जुटायेंगे। उन्हें यह शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि नौसिखिया होने के कारण कोई उनकी वक्तृता सुनने नहीं आता। न अपने को दोष देना पड़ेगा और न लोगों की अभिरुचि को कोसना पड़ेगा। जिन्हें सचमुच ही कुशल वक्ता बनना हो उन्हें इतना झंझट भी ओढ़ना चाहिए। सस्ते में बड़ी उपलब्धियां पाने की फिराक में रहने वाले हर क्षेत्र में असफल रहते हैं। कुशल वक्ता बनने में ही सस्ता सौदा खरीदने वालों को सफलता किस प्रकार मिल सकेगी। प्रवचन कला के सम्बन्ध में कुछ बातें और भी ध्यान रखने योग्य हैं। एक यह कि दो घंटे से अधिक लम्बा आयोजन न खींचा जाय। पैंतालिस मिनट से अधिक लम्बी वक्तृता न दी जाय, अन्यथा लोग ऊबने लगेंगे और ऊब कर चल देंगे। प्रज्ञा पुराण की एक मीटिंग भी डेढ़ घंटे से अधिक की न हों आधा घंटा संगीत, कीर्तन में, पूजा प्रार्थना में लगा देने से विविधता का समावेश हो जाता है और थकने-थकाने वाला भार वहन करने की गुंजाइश नहीं रहती। अग्नि होत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी यही बात है। उसमें एक घण्टे से अधिक समय न लगे इसके लिए इन दिनों प्रचलित हवन पद्धति का और भी अधिक संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है। लोगों की रुझान, अवकाश को ध्यान में न रखा जाय और उन्हें अधिक देर तक रोके रहने का प्रयास किया जाय तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। लोग उस समय भी मन ही मन खीजेंगे और भविष्य में ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होने की उपेक्षा करने लगेंगे।
इसी प्रकार एक बात प्रवचन शैली के सम्बन्ध में और भी ध्यान रखने योग्य है। वह है—धार्मिक भाषणों में गम्भीरता का—एक रसता का प्रवाह बनाए रहना। राजनैतिक मंचों पर से उत्तेजना, आवेश, कर्कशता, अपनाने एवं व्यंग्य आक्रोश व्यक्त करने की गुंजाइश रहती है पर धार्मिक आयोजनों में उसकी गुंजाइश नहीं है। उसमें सौम्य, शान्त, माधुर्य, करुणा एवं भाव संवेदना की सरसता रहनी चाहिए। आक्रोश उत्पन्न करने का तरीका, गरजना, चीखना, गाली-गलौज पर उतारू होना नहीं, वरन् यह है पीड़ित पक्ष की व्यथा से श्रोताओं को करुणार्द्र करने का प्रयत्न किया जाय। साथ ही उन्हें इसके लिए उकसाया जाय कि इस मर्मव्यथा को निरस्त करने में भावनाशीलों की उदार सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार भी उद्देश्य वही पूरा होता है जो भड़काने, और तोड़ फोड़ पर उतारू होने के लिए उत्तेजनात्मक भाषण देने से हो सकता है। आरोप, आक्षेप वाले भाषण वक्ता को जोशीला ठहराते हैं पर साथ ही उसे क्रोधी, झगड़ालू, ठहराकर सहानुभूति भी समेट लेते हैं। यह कठिनाई तब आड़े नहीं आती जब आक्रान्ताओं के पीड़ित पक्ष को जो व्यथा सहनी पड़ी उसे व्यक्त करते हुए श्रोताओं को रुला दिया जाय और उस करुणा के उभार को पीड़ित पक्ष को दूरगामी सहायता में नियोजित किया जाय। इस प्रकार भी आक्रान्ता, आक्रमण और अनीति प्रचलन को उखाड़ने वाला आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। प्रज्ञा अभियान के प्रवक्ताओं की शैली में भी इसी शालीनता का समावेश रहना चाहिए।
वाक् सिद्धि के लिए व्यक्तित्व में भावनात्मक उत्कृष्टता का समावेश करना होता है। साथ ही स्वभाव-व्यवहार में सज्जनोचित शालीनता का गहरा पुट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आत्म संयम और उदार व्यवहार की उभयपक्षीय साधना में चिरकाल तक निरत रहना पड़ता है।
कहा जा चुका है कि वाणी एक शक्ति भी है और एक कला भी। शक्ति तब बनती है जब उसके साथ वक्ता के चिन्तन, चरित्र और व्यवहार की उत्कृष्टता जुड़ गयी हो। कला तब कहलाती है जब बोलने का लहजा, करीना, तरीका, प्रवाह ठीक तरह चलाने का अभ्यास कर लिया जाय। शक्ति और कला का समन्वय होने से चमत्कारी परिस्थितियां सामने आती हैं। मुखर न हो सकने वाली ऋषि वाणी भी अपंग है और मात्र नाटकीय वाचालता सीखी गई हो तो उससे मंच के अभिनेताओं द्वारा कौतुक-कौतूहल उत्पन्न हो सकता है।
युगशिल्पियों की वाक्शक्ति को वाक् सिद्धि स्तर तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए वाणी का संयम अपनाना चाहिए। सामान्य बोलचाल में सचाई, नम्रता, हितकामना का समावेश करते रहा चाहिए। आत्मश्लाघा, क्रोध, विद्वेष, छल, प्रपंच का समावेश रहने पर वाणी अपनी प्रभाव शक्ति खो बैठती है। इसी प्रकार अभक्ष्य खाने वाली जिह्वा भी दग्ध, अपंग स्तर की बन जाती है और विनोद से बढ़कर और कोई गंभीर प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। सरस्वती की साधना यही है कि वाणी का उच्चस्तरीय उपयोग होता रहे। उसे न कहने योग्य न कहने दिया जाय, न खाने योग्य न खाने दिया जाय। इतना बन पड़े तो वाणी के शक्ति रूप में प्रकट होने की संभावना बन गई। शब्द को बाण और व्यक्तित्व को धनुष कहा गया है। दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही निशाना सधता है। यह तथ्य ध्यान में बना रहे तो क्रमशः जीवनक्रम में अधिकाधिक पवित्रता एवं प्रखरता का समावेश करने वाली आत्मसाधना चलेगी और वक्ता की वाणी मंत्र बोलने लगेगी। मंत्र उच्चस्तरीय विचारणा से प्रेरित संभाषण को कहते हैं। मन्त्र की शक्ति सर्वविदित है। मन्त्र सिद्धि और वाक् सिद्धि एक ही तथ्य के दो नाम हैं।
युग सन्धि की वेला में प्रज्ञा-परिजनों को प्रस्तुत महाभारत में अपने अस्त्र-शस्त्र सजाने चाहिए। इसमें सत्परामर्श को ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयुक्त करने की कुशलता इन्हीं दिनों सीखनी चाहिए। सीखने के लिए साधन चाहिए और वातावरण भी। पहलवान बनने के लिए व्यायामशाला, विद्वान बनने के लिए पाठशाला, धनी बनने के लिए उद्योगशाला का आश्रय लिये बिना गति गति नहीं। तैरना सीखने वालों को तालाब में प्रवेश करना होता है। भोजन पकाने के लिए आवश्यक उपकरणों वाला रसोईघर चाहिए। साधनों के अभाव में गायन, वादन, चित्र, प्रतिमा, शिल्प, चिकित्सा आदि किसी भी योग्यता का प्रमाण-परिचय दे सकना संभव नहीं होता। इसलिए वाक् सिद्धि के लिए जहां वक्ता को अपने व्यक्तित्व को, विशेषतया वाणी को संयम-साधना की कसौटी पर खरा सिद्ध करना होता है, वहीं उसकी कला में सौंदर्य, माधुर्य भर देने का अभ्यास भी आवश्यक है। हीरा खरादा जाता है, सोना गलाया जाता है तभी उनकी विशिष्टता निखरती है। आभूषण बनने की स्थिति तक उन्हें अनेक बार—अनेक प्रकार से संस्कारित किया जाता है। वाणी को सुसंस्कारी बनाने का प्रयास भी इसी प्रकार होना चाहिए।
अभ्यास की अपनी आवश्यकता है। कला के रूप में वाणी को परिष्कृत करने के लिए तदनुरूप अवसर चाहिए। इसके लिए श्रोताओं की उपस्थिति एवं मनःस्थिति में उर्वरता होनी चाहिए, अन्यथा बोया गया बीज ऐसे ही सड़ेगा-घुनेगा और चिड़ियों के पेट में चला जायगा। उसे अंकुरित-पल्लवित होने का अवसर ही न मिलेगा। ऐसे श्रोता भी हमें अपने ही प्रयत्न से जमा करने होंगे। दूसरों द्वारा एकत्रित की गई भीड़ उन्हीं के स्तर तथा रुझान की होगी जैसी कि संयोजकों की है। अपने प्रयोग अभ्यास के लिए हमें अपने ही स्तर का जन-समुदाय एकत्रित करना चाहिए और उस एकत्रीकरण में भी दूसरों का मुंह ताकने की अपेक्षा स्वयं ही पराक्रम-पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरे भीड़ जुटायें, मंच बनायें और उस पर अपने से जा विराजने का अनुरोध करें। इस आशा में बैठे रहने पर कदाचित् ही वैसा अवसर कभी मिलेगा; क्योंकि आयोजन कभी-कभी ही किन्हीं के प्रयत्न से बहुत समय बाद सम्पन्न होते हैं। उनमें भी यह विश्वास नहीं कि अपने को बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं। ऐसी दशा में उचित यही है कि जितनी उत्कंठा अपनी बात लोगों को सुनाने; गले उतारने की है उतनी ही चेष्टा आयोजन के सूत्र संचालन के निमित्त की जाय। युग-शिल्पियों को न केवल वक्ता वरन् समुदाय को एकत्रित कर सकने में समर्थ संयोजक भी होना चाहिए।
प्रज्ञा अभियान के अन्तर्गत वर्ष में कई बार कई स्थानीय आयोजन करने के लिए कहा गया है। इन्हें पर्व आयोजन कहा गया है। वसन्त पंचमी, होली, गायत्री जयन्ती, गुरुपूर्णिमा, श्रावणी, दिवाली ऐसे ही पर्व हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मनाया जाना चाहिए। इन आयोजनों के साथ व्यक्ति, परिवार और समाज की उच्चस्तरीय संरचना में भारी योगदान देने वाली प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि उन्हें सामूहिक रूप से मनाया जाय और उस तथ्य का स्मरण दिलाया जाय जिनमें शालीनता बनाये रहने और सत्प्रयत्नों के लिए पराक्रम करने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए किस प्रक्रिया को किस प्रकार अपनाया जाय। इस विस्मृत पक्ष को इन दिनों विशेष रूप से उभारा जाना चाहिए। प्रयत्न यह होना चाहिए कि पर्व मनाने की सामूहिक विधि-व्यवस्था को नये सिरे से पुण्य परम्परा का एक रूप दिया और उसमें सम्मिलित रहने के लिए सर्वजनीन उत्साह उत्पन्न किया जाय।
युग सृजन के प्रवक्ताओं को वाक् शक्ति का व्यापक उपयोग करने के लिए मात्र कथन की एकांगी कार्यपद्धति अपनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें दो मोर्चों पर दुधारी तलवार लेकर जूझना पड़ेगा। एक कार्य यह कि वे वाणी के कलाकार बनें और उसे प्रभावी बनाने के लिए अपने चरित्र-चिन्तन को उच्चस्तरीय बनावें। दूसरा यह कि श्रवणकर्त्ताओं को जुटायें। उनमें इस प्रकार की अभिरुचि उत्पन्न करें। यह दोनों ही कार्य सम्पन्न कर सकने वाले ही कुशल वक्ता की भूमिका निभा सकेंगे। जो इन दो प्रसंगों के साथ जुड़े हुए दो-दो कार्यक्रमों में से एक को भी महत्वहीन समझेंगे, एक की भी उपेक्षा करेंगे वे वाचाल भले ही कहला सकें, नव-युग के प्रवक्ता नहीं कहे जा सकेंगे। हमें एकांगी प्रयास से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वरन् समग्र प्रयास का संयोजक होना चाहिए।
वाणी में शक्ति उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसमें कलाकारिता का समावेश कैसे हो सकता है—इस पर पिछली पंक्तियों में सैद्धान्तिक प्रकाश डाला जा चुका है; उसका व्यवहार तो हर व्यक्ति को अपनी मनःस्थिति और परिस्थिति देखते हुए स्वयं ही निर्धारित करना होगा। किसके चरित्र-चिन्तन में क्या कमी है और उसे सुधारने के लिए किन परिस्थितियों में किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है—इसका निर्धारण अन्य व्यक्ति कदाचित ही कर सकें। कुछ सहायक वे हो सकते हैं जो साथ रहते हैं और स्थिति के साथ तालमेल बिठाने वाला परामर्श दे सकते हैं। हर वक्ता को विचारशील होना चाहिए। जन मानस को—लोक प्रवाह को सुधारने की जिम्मेदारी उठाने वालों में इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व को इस ढांचे में ढालें कि वे सच्चे अर्थों में सरस्वती के उपासक, वाक्शक्ति के धनी और लोक मानस को उलट सकने में समर्थ सिद्ध हो सकें। बड़े वरदान पाने के लिए बड़ा तप करना चाहिए। यह साधना का विषय है, उसमें धैर्य और संकल्प का समान रूप से प्रयोग करना पड़ेगा और बन्दर वृत्ति जैसी चंचलता को एक कोने पर रखकर एकाग्र-एकनिष्ठ बनने के लिए प्रयत्नरत होना पड़ेगा। यह एक पक्ष ऐसा है जो एकांकी संयोजन और प्रयत्न के आधार पर स्वयं ही सम्पन्न किया जा सकता है; दूसरों के सहयोग की इसमें नगण्य-सी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा प्रयास थोड़ा कठिन है। उसमें न दूसरों से सम्पर्क साधने की, उन्हें सहमत करने, सहयोगी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। श्रोता जुटाना बड़ा काम है। दूसरे क्यों किसी की मर्जी पर चलें? क्यों अपना समय किसी की इच्छापूर्ति के लिए दें? विशेषतया तब, जबकि अपनी योग्यता उतनी नहीं उठ सकी कि श्रोता बहुत कुछ पाने की आशा से एकत्रित हों और बहुत दिनों तक- बहुत समय तक उसके लिए आते रहें। अभ्यास में प्रवीणता एक दिन में तो आती नहीं। उसके लिए सहयोगी श्रोता न जुट सकें तो समझना चाहिए कि गाड़ी का एक पहिया टूट गया। उड़ने के लिए आवश्यक दो पंखों में से एक कट गया। एक हाथ से ताली कैसे बजेगी?
चूहा अपना बिल स्वयं खोदता है पर सांप बने बिल में घुस पड़ने की घात लगाता है। हमें सांप नहीं चूहा बनना चाहिए। दूसरों के आयोजित सम्मेलनों की ताक में रहने और जित-तिस के द्वारा बनाये मंचों पर जो विराजने वाली ललक है वह है तो सरल और सुनहरी, पर उसे व्यावहारिक नहीं मानना चाहिए। जिनने अपने मंच बनाये, सम्मेलन बुलाये हैं, वे उपस्थिति को प्रसन्न करने वाले वक्ता बुलाते हैं। जिनसे पैसा लिया है, जिनने समय दिया है उनकी मर्जी पूरी न करने पर आगे का रास्ता बन्द होता है। इसलिए विभिन्न संयोजक सदा मूर्धन्यों को बुलाते हैं और नौ सिखियों का पत्ता काटते हैं। फिर वे यह भी देखते हैं वक्ता लोकरुचि के अनुरूप बोलने का अभ्यस्त है या नहीं। अपना मिशन लोकरुचि से विपरीत न सही भिन्न तो है ही। ऐसी दशा में लोकरुचि को प्रधानता देने वाले संयोजक उसी प्रकार की व्यवस्था बनाते और वैसे ही वक्ता बुलाते हैं। हमें अपना ही कुआं खोदना और अपने हाथ से खींचा पानी पीने की तैयारी करनी चाहिए।
जिन दिनों चाय का प्रचलन नहीं था, उन दिनों उसके प्रचारक घर-घर जाते थे। हाथों में गरम चाय की बन्द बाल्टी और गिलास कुल्हड़ होते थे। सवेरा होते-होते घरों पर पहुंचते, दरवाजे खटखटाते, आवाज लगाते थे—गरम चाय पीने की। ‘‘चाय पियो-बहुत दिन जियो’’का नारा लगाते थे और जो थोड़ी भी रुचि लेता था उसे मुफ्त चाय पिलाते थे। जो अच्छी लगने की बात कहता उससे एक पैसे वाला चाय का पैकेट खरीदने का अनुरोध करते। बनाने की विधि सिखाते और कहते इस एक पैकिट में चार कप उम्दा चाय घर पर बन सकती है। उसे पीने से क्या-क्या लाभ होते हैं यह बताने का वे तब तक क्रम जारी रखते थे जब तक कि सहमति सूचक सिर न हिलने लगता। इन चाय प्रचारकों के स्टॉल हाट-बाजारों में पहुंचते और उधर घूमने-फिरने वाली भीड़ को आकर्षित करके वही उपक्रम चलाते जो आये दिन घर-घर जाकर करना पड़ता। यह जन सम्पर्क ही था जिसके कारण चाय अन्न-वस्त्र की तरह अपना स्थान अनिवार्य दैनिक आवश्यकताओं में बना लिया है। भोर होने से पहले और बहुत रात बीते तक स्टालों पर भीड़ लगी रहती है।
युगान्तरीय-चेतना के प्रति वर्तमान स्थिति में उपेक्षा स्वाभाविक है। हर अजनबी सुधारवादी प्रस्तुतीकरण का प्रारंभ में उपहास-तिरस्कार होता रहा है। बहुत दिन बाद ही सतत प्रयास से प्रवाह को मोड़ना सम्भव हुआ है। यही बात वर्तमान लोक मानस के सम्बन्ध में भी है। उससे अपरिचित तथ्यों से परिचित कराने से लेकर सहमत बनाने तक की लम्बी मंजिल युग-शिल्पियों को ही पूरी करनी पड़ेगी। वक्तृता का उपयोग सही लोगों में सही स्तर पर हो सके, इसके लिए चाय प्रचारकों की नीति अपनानी पड़ेगी। उस लम्बी भूमिका के निर्वाह में जितनी प्रगति होगी उतना ही सफलता का पथ प्रशस्त होगा।
प्रज्ञा अभियान के आरंभिक दो प्रयोगों में से एक है घर-घर हर शिक्षित को नियमित रूप से प्रज्ञा साहित्य पढ़ाने और वापिस लेने के लिए जाना। ज्ञान रथ इसी के लिए जगह-जगह बनाये और चलाये जा रहे हैं। दूसरा प्रयोग है स्लाइड प्रोजेक्टर। मोहल्ले-मोहल्ले प्रकाश चित्रों को दिखाते हुये युगान्तरीय चेतना का आलोक जन-जन के मन-मन में प्रवेश करना। इसमें लोकरंजन और लोक मंगल दोनों का समन्वय होता है और जनता को एकत्रित करने में कहीं भी कठिनाई नहीं पड़ती। मुहल्ले के बाल-वृद्ध, नर-नारी सहज ही उस विनोद कौतूहल को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। इन दोनों प्रयोगों में वक्तृत्व कला के अभ्यासी को भाषण और संभाषण दोनों का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। घर-घर साहित्य देने वापिस लेने के लिए जाने पर कुछ तो पूछना बताना ही पड़ेगा। पोस्टमैन की तरह तार चिट्ठी फैलाकर तो चल नहीं देना है। अपना प्रयोजन और पुस्तकों का माहात्म्य बताये बिना तो पढ़ने वालों की अभिरुचि ही नहीं जगेगी। साहित्य प्रसार की प्रक्रिया में संभाषण कला का अभ्यास करने और उसे विकसित और परिष्कृत करने की पूरी-पूरी गुंजाइश है। जन सम्पर्क साधने से ही समर्थन और सहयोग प्राप्त करने की सफलताओं का दर्शन हो सकेगा। सम्पर्क साधने में प्रज्ञा-साहित्य का प्रचार सर्वोत्तम है। इसमें देना ही देना है लेना कुछ नहीं। ऐसी प्रक्रिया लोकप्रिय क्या न होगी? इसमें निरत लोगों को सहानुभूति क्यों नहीं मिलेगी? कृतज्ञता का लाभ निश्चित रूप से लौट कर मिलेगा।
इसी प्रकार दूसरे प्रयोग ‘स्लाइड प्रोजैक्टर’ में भाषण कला का अभ्यास अनवरत रूप से चलता रहा सकता है। आज इस मुहल्ले तो कल उस मुहल्ले की योजना बना लेने पर पूरे वर्ष यह कार्यक्रम चलता रह सकता है। एक वर्ष की स्लाइडें जब तक पूरी होती हैं तब तक नये वर्ष के अगले चित्र बन कर आ जाते हैं और यह चलता फिरता सिनेमा, नई-नई फिल्म स्लाइडें दिखाते हुये अपनी प्रचार प्रक्रिया का निश्चित रूप से गतिशील रखे रह सकता है। भाषण-कला के अभ्यास में जनता को एक एकत्रित करने का इससे सरल, सस्ता, आकर्षक और सुनियोजित तरीका और कोई हो ही नहीं सकता।
यह चलती फिरती प्रक्रिया हुई। इससे आगे का सभा—सम्मेलनों का—विचार गोष्ठियों का वह स्वरूप बनता है जिसमें मंच से बोलने की प्रक्रिया सधती है। इसमें जन्मदिवसोत्सव मनाने की बात पहले कही जा चुकी है। इस स्तर के आयोजन अपनी मित्र मंडली से आरंभ किये जा सकते हैं और किसी को भी प्रोत्साहित करके, इस हर्षोत्सव के लिए बात की बात में सहमत किया जा सकता है। दो चार रुपये खर्च करने जैसी छोटी सी व्यय व्यवस्था निर्धन से निर्धन भी वहन कर सकता है विशेषतया तब, जब उसे हीरो बनने का अवसर मिलता है, और घर पर मित्र सम्बन्धियों को एकत्रित होने का आनन्द मिलता है। आतिथ्य खर्चीला न होने पाये, इस प्रतिबन्ध से यह कार्यक्रम नितान्त सरल हो गये हैं। हवन की प्रक्रिया इतनी सरल सस्ती बना दी गयी है कि वह एक दो रुपये में ही अच्छा खासा वातावरण बनाने और उत्साह उत्पन्न करने की आवश्यकता पूरी करती है। यदि अपना निश्चय हो तो सप्ताह में एक आयोजन का प्रबंध अपने एकाकी प्रयत्न से- अपने ही सम्पर्क क्षेत्र में भली प्रकार हो सकता है। वक्तृता के लिए मंच तैयार मिल गया न? महिलाएं यह कार्य महिलाओं का जन्म दिन मनाकर—बच्चों के षोडश संस्कारों की योजना बना कर अपने क्षेत्र में मूर्धन्य बन सकती हैं और वक्तृता के अभ्यास में निपुण हो सकती हैं।
पर्व आयोजन इससे बड़ी और अधिक प्रभावी योजना है। वसन्त, होली, गायत्री जयंती (गंगा दशहरा), गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, सिद्ध अमावस्या, दीवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि पर्वों की छुट्टियां होती ही हैं। लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर इन प्रयोजनों के पीछे उद्देश्य क्या है। इन पर्वों पर रात्रि को या प्रातः काल जब स्थानीय सुविधा दीखे, एक छोटा पर्व आयोजन किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा धार्मिक कर्मकाण्ड मिला रहने से वातावरण में श्रद्धा का पुट लगता है। और साथ ही लोक शिक्षण की विभिन्न दिशा धाराओं पर प्रकाश डालने का इन पर्वों पर सहज अवसर मिलता है। इन आयोजनों के लिए वक्तृत्व कला के अभ्यासी को स्वयं भी प्रयत्नरत रहना चाहिए और साथी सहयोगियों की सहायता से उसे आकर्षक, सफल बनाने में जुटना चाहिए। यह प्रवाह उलटने की दृष्टि से तो महत्व पूर्ण है ही, अभ्यासी को अपने लिए स्वनिर्मित मंच खड़ा करने और अभ्यास बढ़ाने का भी सुयोग सहज ही मिलता है। बड़े सम्मेलनों में बड़े वक्ता की तलाश होती है पर जन्म दिवसोत्सव और पर्वों की मुहल्ला गोष्ठियों में तो आरम्भिक वक्ता भी मान-सम्मान पाता है।
दूसरे बड़े आयोजन नवरात्रियों के साधना पर्व हैं। इन नौ दिन लगातार चलने वाले सामूहिक धर्मानुष्ठान आयोजनों में जो भागीदार बनते हैं, नियमित रूप से उपस्थिति होते ही हैं। साथ ही पांच अन्य साथियों को घसीट कर लाने की बात भी उनकी पुण्य प्रक्रिया में सम्मिलित की गयी है। इस आधार पर बसी अनुष्ठान कर्ता अपने साथ सौ और समेट लाते हैं। कुछ इधर उधर के आ जाने से डेढ़ दो सौ की उपस्थिति पूरे नौ दिन तक बनी रहती है। वर्ष में दो बार यह अवसर आते हैं। गायत्री के माध्यम से प्रज्ञा अभियान के समस्त प्रतिपादनों को उपस्थित समुदाय को हृदयंगम कराने में सुविधा होती है। ऋतम्भरा गायत्री की साधना और प्रज्ञा-अभियान की युगान्तरीय चेतना एक ही तथ्य के दो रूप हैं। दोनों का समन्वय बड़ी सरलता और सुन्दरता के साथ निभ जाता है। नव रात्रि सत्रों के अन्यान्य अनेकों लाभ है। उनमें से एक लाभ यह भी है कि वक्तृत्व कला के अभ्यासी स्थानीय आयोजनों में विचार व्यक्त करते-करते इतने अभ्यस्त निपुण बन सकते हैं कि बृहत् सम्मेलनों में प्रमुख वक्ता की आवश्यकता पूर्ण कर सकने में सफल हो सकें।
जहां बोलने में अड़चन पड़ती हो विचारों का तारतम्य न बैठता हो वहां पढ़कर सुना देना भी एक उपाय है। युग साहित्य जिन हाथों से लिखा जा रहा है उसमें जो आग रहती है उसकी समीपता तथा गर्मी सभी को रुचती है। यह कहा जाय कि एक प्रेरणा स्रोत के अन्तराल से निकली ऊर्जा को उपस्थित लोगों तक पहुंचाने, उससे अवगत कराने भर का विनम्र प्रयास किया जा रहा है तो उपस्थित लोग किसी लेख को सुनने के लिये भी उतने ही उत्साह से तैयार रहते हैं कितना कि स्थानीय वक्ता का भाषण सुनने के लिए। छपे को पढ़कर सुना देने में भी कलात्मक उभार लाने पड़ते हैं। इस भाव अभिनय के लिए इस प्रकार सुनाये जाने वाले भाषणों में अधिक गुंजाइश रहती है। क्योंकि इनमें कुछ सोचने याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही प्रवाह क्रम बिगड़ने जैसी अड़चन भी सामने नहीं आती। ज्ञान गोष्ठियों में इस प्रकार लेख या पुस्तकों का अंश सुना देने का भी कम से कम प्रज्ञा परिजनों को तो अवसर है ही। वे इसे सुनने में जिस हस्ती का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे उस वक्तृता में भागीदार रखने से जहां अपना वजन हल्का होता है वहां भी उसकी प्रभावशक्ति में कोई कमी नहीं आती।
वक्तृता के अभ्यास के लिए दूसरा चरण यही है कि अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति हो और सुनने और समझने के लिए पूर्व भूमिका ऐसी हो जिसमें सुनने वालों को अपनी मर्जी के विपरीत सुनने पर अनख न लगे, अरुचि उत्पन्न न हो और बीच में ही उठ चलने जैसी कुरुचिपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न न हो। इस उपचार को जो भी अपनायेंगे उसे भाषण शिक्षा का एक अनिवार्य अंग मानेंगे और अपने श्रोता आप जुटायेंगे। उन्हें यह शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि नौसिखिया होने के कारण कोई उनकी वक्तृता सुनने नहीं आता। न अपने को दोष देना पड़ेगा और न लोगों की अभिरुचि को कोसना पड़ेगा। जिन्हें सचमुच ही कुशल वक्ता बनना हो उन्हें इतना झंझट भी ओढ़ना चाहिए। सस्ते में बड़ी उपलब्धियां पाने की फिराक में रहने वाले हर क्षेत्र में असफल रहते हैं। कुशल वक्ता बनने में ही सस्ता सौदा खरीदने वालों को सफलता किस प्रकार मिल सकेगी। प्रवचन कला के सम्बन्ध में कुछ बातें और भी ध्यान रखने योग्य हैं। एक यह कि दो घंटे से अधिक लम्बा आयोजन न खींचा जाय। पैंतालिस मिनट से अधिक लम्बी वक्तृता न दी जाय, अन्यथा लोग ऊबने लगेंगे और ऊब कर चल देंगे। प्रज्ञा पुराण की एक मीटिंग भी डेढ़ घंटे से अधिक की न हों आधा घंटा संगीत, कीर्तन में, पूजा प्रार्थना में लगा देने से विविधता का समावेश हो जाता है और थकने-थकाने वाला भार वहन करने की गुंजाइश नहीं रहती। अग्नि होत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी यही बात है। उसमें एक घण्टे से अधिक समय न लगे इसके लिए इन दिनों प्रचलित हवन पद्धति का और भी अधिक संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है। लोगों की रुझान, अवकाश को ध्यान में न रखा जाय और उन्हें अधिक देर तक रोके रहने का प्रयास किया जाय तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। लोग उस समय भी मन ही मन खीजेंगे और भविष्य में ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होने की उपेक्षा करने लगेंगे।
इसी प्रकार एक बात प्रवचन शैली के सम्बन्ध में और भी ध्यान रखने योग्य है। वह है—धार्मिक भाषणों में गम्भीरता का—एक रसता का प्रवाह बनाए रहना। राजनैतिक मंचों पर से उत्तेजना, आवेश, कर्कशता, अपनाने एवं व्यंग्य आक्रोश व्यक्त करने की गुंजाइश रहती है पर धार्मिक आयोजनों में उसकी गुंजाइश नहीं है। उसमें सौम्य, शान्त, माधुर्य, करुणा एवं भाव संवेदना की सरसता रहनी चाहिए। आक्रोश उत्पन्न करने का तरीका, गरजना, चीखना, गाली-गलौज पर उतारू होना नहीं, वरन् यह है पीड़ित पक्ष की व्यथा से श्रोताओं को करुणार्द्र करने का प्रयत्न किया जाय। साथ ही उन्हें इसके लिए उकसाया जाय कि इस मर्मव्यथा को निरस्त करने में भावनाशीलों की उदार सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार भी उद्देश्य वही पूरा होता है जो भड़काने, और तोड़ फोड़ पर उतारू होने के लिए उत्तेजनात्मक भाषण देने से हो सकता है। आरोप, आक्षेप वाले भाषण वक्ता को जोशीला ठहराते हैं पर साथ ही उसे क्रोधी, झगड़ालू, ठहराकर सहानुभूति भी समेट लेते हैं। यह कठिनाई तब आड़े नहीं आती जब आक्रान्ताओं के पीड़ित पक्ष को जो व्यथा सहनी पड़ी उसे व्यक्त करते हुए श्रोताओं को रुला दिया जाय और उस करुणा के उभार को पीड़ित पक्ष को दूरगामी सहायता में नियोजित किया जाय। इस प्रकार भी आक्रान्ता, आक्रमण और अनीति प्रचलन को उखाड़ने वाला आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। प्रज्ञा अभियान के प्रवक्ताओं की शैली में भी इसी शालीनता का समावेश रहना चाहिए।
Write Your Comments Here:
- व्यक्तित्व सम्पन्न वक्ता का प्रभावी प्रवचन
- काया की सशक्त प्रयोगशाला और शब्द शक्ति की ऊर्जा
- वाणी की शक्ति एवं प्रखरता
- वाणी में सामर्थ्य का उद्भव
- भाषण कला का आरम्भ और अभ्यास
- वक्ता को अध्ययनशील होना चाहिए
- सरल भाषण की कसौटी
- भाषण और भावाभिव्यक्ति का समन्वय
- सभा मंच पर जाने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखें
- भाषण का स्तर गिरने न दें
- आरम्भिक कठिनाई का समाधान आधी सफलता
- प्रगति इस प्रकार संभव होगी
- अभ्यास क्रम के लिए सुगम अवलम्बन
- श्रोताओं को नियमित रूप से उपलब्ध करने की सरल प्रक्रिया
- वक्ताओं को ही श्रोता भी जुटाने पड़ेंगे
- संभाषण के कुछ सारगर्भित सिद्धान्त
- मात्र भाषण ही नहीं साथ में गायन भी