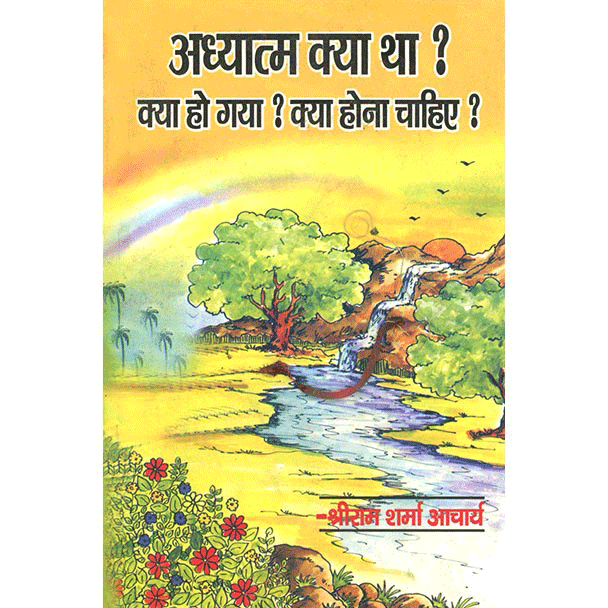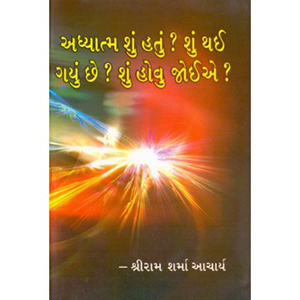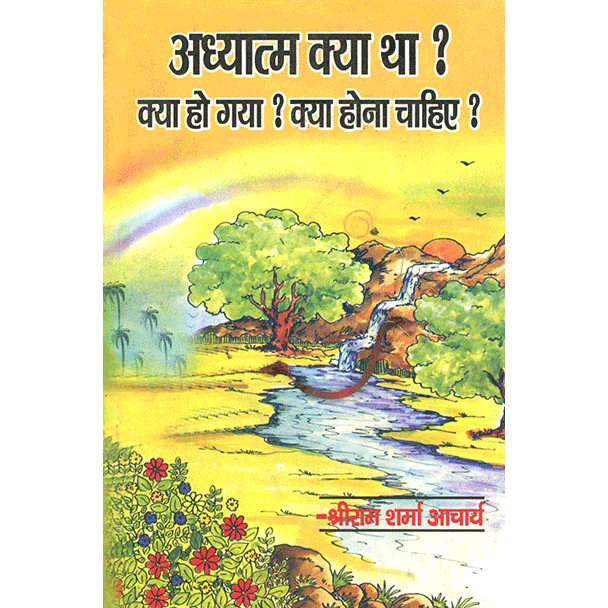अध्यात्म क्या था? क्या हो गया? क्या होना चाहिए? 
समग्र जीवन को अध्यात्म से ओत प्रोत करें
Read Scan Versionईश्वर के स्वभाव, स्वरूप एवं विधान के संबंध में जितनी भ्रान्तियां लोगों में हैं उससे भी अधिक साधक के स्तर एवं साधना विधान, समय और मार्गदर्शक जैसे संबंधित प्रसंगों में भी हैं।
उपनिषदों ने निराकार ब्रह्म का स्थान हृदय गुफा और स्वरूप अंगुष्ठ मात्र ज्योति वाले आकार का लिखा है। यह ध्यान और भावना का विषय है। अन्तर्मुखी होकर ध्यान मग्न स्थिति में इस प्रकार की भावना परिपक्व की जाती रहे तो आत्म साक्षात्कार की विधा चल पड़ती है। अंतरंग में ही ईश्वर का निवास है और उसके घर को शरीर को देवालय जैसा पवित्र बना कर रखा जाय, आत्म निर्भर रहा जाय आत्म परिष्कार में जुटा जाय, यह ईश्वर दर्शन का निराकार मार्ग है।
साकार दर्शन का आग्रह अर्जुन को, यशोदा को, कौशिल्या को, काकभुशुण्डि आदि को था। इन सभी को भगवान ने अपना प्रत्यक्ष शरीर विराट विश्व के रूप में अनुभव कराया और उसकी साधना के लिए लोक मंगल के परमार्थ कार्यों में सत्प्रवृत्ति संवर्धन की सेवा साधना में निरत होने के रूप में समझाया।
साधनात्मक कर्मकाण्डों का उद्देश्य भी वही है कि उन माध्यमों को अपनाकर आत्म चेतना को श्रेष्ठ समुन्नत बनाया जाय। ईश्वर स्मरण के निमित्त किये गये जप ध्यान का उद्देश्य है कि जीवन दानी को, उसकी आकांक्षा को, धरोहर को ध्यान में रखते हुए जीवनचर्या की उदात्त योजना बनाई जाय, चंदन के माध्यम से वातावरण को सुविकसित करने का, अक्षत के माध्यम से अंशदान का, दीप के माध्यम से सद्ज्ञान का आलोक हृदयंगम कराने एवं सुविकसित जैसे कार्यों की प्रेरणा ग्रहण करने का निर्धारण है। यह समग्र शालीनता ही ईश्वर की प्रसन्नता का केन्द्र बिन्दु है।
साधना में श्रद्धा प्रमुख है। श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर बताते हुए रामायण में कहा गया है कि इन दोनों का प्रथम आश्रय लेना पड़ता है। इसके उपरान्त ही परम सिद्धि का आधार बनता है। मीरा के गिरधर गोपाल, राम कृष्ण परम हंस की काली, एकलव्य के मृत्तिका विनिर्मित द्रोणाचार्य इसके प्रमाण हैं कि श्रद्धा का आरोपण करके किसी भी माध्यम को सिद्धि प्रदान करने के माध्यम हैं। पत्थर के खिलौने को इस श्रद्धा के आधार पर ही देव रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। श्रद्धा के अभाव में तो वह खिलौना मात्र बन कर रह जाता है। यही बात मंत्र के संबंध में भी विश्वास हो तो मंत्र अन्यथा अक्षरों की रटन्त। देवता में, मंत्र में जो सामर्थ्य प्रकट होती है वह वस्तुतः साधक की श्रद्धा ही महान बन कर प्रकट होती है। ईश्वर हमारी ही प्रतिच्छाया और प्रतिध्वनि है। यह ठीक है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या यह भी गलत नहीं है कि उसे मनुष्य की श्रद्धा ने ही अपने सांचे में ढाला है। अन्य जीव जन्तुओं में से तो किसी को ईश्वर का भान अनुभव होता ही नहीं।
धनुष की प्रत्यंचा कड़ी और सही होने पर ही तीर की दूरी और चोट प्रभावी होती है। अन्यथा बेचारे तीन को चुभाने पर तो छोटा सा गड्ढा ही हो सकता है। साधक का व्यक्तित्व ही साधना को सशक्त बनाता है। वह घटिया और ओछा हो तो शब्दों की रटन्त भर से क्या कुछ बनने वाला है। वाल्मीकि उलटा नाम जपने से भी सिद्ध पुरुष हो गये थे। और राम के घर में निवास करने वाली कैकेयी, मंथरा आदि को अपयश ही हाथ लगा था। राम से बड़ा राम का नाम बताने वाली उक्ति सही है। राजकुमार राम तो अपने सम्पर्क वालों को ही प्रभावित करते थे। पर राम नाम तो अभी भी लोगों को तारता है। गांधी जी जैसों का इष्ट बनता है। कारण कि उसके साथ श्रद्धा जुड़ी होती है। जो मिट्टी के ढेले को भी पूजा प्रयोजनों में देवाधिदेव गणेश बना देती है।
गुरु के अनुग्रह या मार्ग दर्शन की बात को सर्वत्र बहुत महत्व दिया गया है। कभी-कभी तो उसे गोविन्द से भी बढ़कर बताया जाता है। इसकी तलाश में बहुत लोग रहते हैं और इस फिराक में रहते हैं कि कोई सिद्ध
पुरुष मिले तो हमें पार लगावें। पर वे यह भूल जाते हैं कि नदी की सतह पर लकड़ी की नाव ही चल सकती है। पत्थर का टुकड़ा तो उसमें डालते ही डूब जाता है। स्मरण रहे इस दुनिया में सुयोग्यों की, दाताओं की कमी नहीं वे प्यासे से फिरते हैं कि कौन सत्पात्र मिले और किसे अपनी परम्परा सौंपकर देव ऋण से उऋण हों; किन्तु सत्पात्र न मिलने पर दुरुपयोग के लिए कोई अपनी परिश्रम की कमाई कुपात्र के हाथों किसलिए सौंपेंगे? इस अनुग्रह से तो उसमें अहंकार और विनाश कृत्य ही बढ़ेगा। रावण, कुम्भकरण, मारीच, हिरण्यकश्यपु, वृत्तासुर, भस्मासुर, महिषासुर आदि असुर कठिन साधना करके ऊंचे वरदान पाने में भी सफल हो गये; पर उस उपलब्धि से उनका कुछ बना नहीं। बिगड़ा ही है।
कन्या का पिता अपनी सुयोग्य लाड़ली बेटी के सयानी हो जाने पर कोई तदनुरूप सुयोग्य लड़का ढूंढ़ने के लिए दूर-दूर तक खोज बीन करता है। मिल जाने पर अपने भाग्य को सराहता है पर यदि कोई कुपात्र लड़की के पिता से प्रार्थना करे कि इस लड़की को हमें दे दें तो उसे दुत्कार ही पड़ेगी। सिद्ध पुरुष इतने मूर्ख नहीं होते कि किसी स्वार्थी और ओछे आदमी की वस्तु स्थिति न परख सके और ऐसे ही अपनी गाढ़ी कमाई तप साधना को चापलूसी मात्र के बदले लुटा दें।
आत्मा की प्रगति क्रमिक गति से होती है। उसमें समय लगता है और धैर्य रखना पड़ता है। चौरासी लाख योनियों के कुसंस्कारों का परिशोधन करने के लिए कुछ जन्म लगें तो इसमें अधीर नहीं होना चाहिए। पानी के बबूले की तरह फूलना और झाग की तरह बैठ जाना जैसी उक्ति चरितार्थ नहीं करनी चाहिए। शिव के सहस्र वर्ष की समाधि लगा लेने पर पार्वती ने अपना निश्चय बदला नहीं था। परीक्षा के लिए सातों ऋषियों को एक ही उत्तर दिया था—‘‘कोटि जनम लगि रगर हमारी। बरउं शंभु न त, रहउं कुमारी।।’’ धैर्य संकल्प और साहस ही साधक की निधि है जिसके पास वह है उसका देर सवेर में लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित ही है। उतावले ही अधीर होते, निराशा व्यक्त करते और अपनाया हुआ मार्ग छोड़ते हैं। इन सभी तथ्यों को हृदयंगम कर लेना हर सच्चे साधक के लिए आवश्यक है।
दैवी शक्तियां और सिद्धियां मिलती तो हैं पर उनके साथ एक शर्त जुड़ी होती है कि उनका उपयोग लोभ, मोह या अहंकार की पूर्ति के लिए न किया जाय वरन् उन्हें पूरी तरह मात्र परमार्थ के लिए सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए ही खर्च किया जाय। तृष्णा, लिप्सा की पूर्ति के लिए यदि कुछ आवश्यक है तो वह अपने श्रम, बुद्धिबल या कौशल से कमाया जाना चाहिए। सन्तों का तप या देवताओं का अनुग्रह उनके लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए जो विश्व वाटिका को सींचने समुन्नत करने में संलग्न हैं। उनका हक वे लोग क्यों हड़पे जो अपनी ही सुविधा, सम्पन्नता के लिए उन्हें भक्त शिष्य का ढोंग बना कर हथियाना चाहते हैं।
साधना का स्वरूप है जीवन की सर्वतोमुखी उत्कृष्टता। उसके ही स्वरूप में अपने व्यक्तित्व का अनुकरणीय, अभिनंदनीय और प्रेरणाप्रद बनना। दूसरा यह कि विश्व वाटिका को समुन्नत बनाने में अपने श्रम, समय तथा साधनों का उदारतापूर्वक समर्पण करना। जो इस राजमार्ग पर चलते हैं उन्हें हाथों हाथ उसका प्रतिफल मिलता है। आत्म संतोष लोक सम्मान एवं सहयोग के साथ ही दैवी अनुग्रह की अदृश्य लोकों से अनुदान वर्षा। इतना पाकर कोई भी कृत कृत्य हो सकता है। संग्रही विलासी और अहंकार तो एक प्रकार के उन्मादी होते हैं। उनकी खुमारी बढ़ाने और दुर्गति कराने के लिए उच्चस्तरीय शक्तियां अपने अनुदान को वरदान के रूप में देती नहीं। गिरते के गले में पत्थर बांधने की कृपा कोई क्यों करे? जिससे उसका पतन और भी सुनिश्चित हो जाय।
यही हैं वे मोटे सिद्धान्त जिन्हें अध्यात्म साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चय करने के पूर्व ही समझ लेना चाहिए।
अध्यात्म प्रवृत्तियां अपनाने पर संसार को भव बन्धन माया मिथ्या बताने जैसे दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। न इधर उधर भटकने तथा भिक्षा पर निर्वाह करने की। अपने युग के आदर्श सन्तों में गांधी बिनोवा की नीति सर्वोपरि है। सामान्य वेष भूषा में रहते हुए सादा जीवन उच्च विचारों की नीति को पाला जाय इतना ही पर्याप्त है। कन को लोभ, मोह, अहंकार की कुत्साओं में न भटकने दिया जाय तो छोटे परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह कुछ भी कठिन नहीं पड़ता। परिजनों को स्वावलम्बी सुसंस्कारी बनाया जाय तो उनके लिए उत्तराधिकार में प्रचुर सम्पदा छोड़ मरने की जरूरत नहीं है। तारतम्य ऐसा बिठाना चाहिए कि आधी आयु पारिवारिक आजीविका सम्बन्धी कार्यों में लग कर शेष आधा जीवन वानप्रस्थ स्तर के परमार्थ कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आज की परिस्थितियों में और सर्वोपरि महत्व एवं प्राथमिकता देने योग्य एक ही परमार्थ है जन मानस का परिष्कार। इसी के निमित्त जन सम्पर्क साधा और घर-घर अलख जगाना चाहिए।
प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी को अपने जीवन का स्वरूप ब्राह्मण साधु जैसा बनाना चाहिए। इन्हीं परम्पराओं के जीवंत रहने के कारण व्यक्तित्ववान लोकसेवकों का बड़ा समुदाय उद्भूत होता रहता था और उनके द्वारा देश की ही नहीं समस्त संसार की भावनात्मक संरचना बन पड़ती थी। इन्हीं सेवा साधनाओं के फलस्वरूप भारत जगद्गुरु बना था और उसके अजस्र अनुदानों को विश्व के हर क्षेत्र में भूरि-भूरि सराहा गया था। देव मानवों की उत्पत्ति साधु ब्राह्मण परम्परा द्वारा ही संभव हुई थी। इसी खदान में से बहुमूल्य नर रत्न निकलते रहे थे। आज ब्राह्मण वंश और साधु वेश भर जीवित रह गया है। उसकी विशिष्टतायें और वरिष्ठतायें एक प्रकार से तिरोहित ही हो गईं। इस कारण न केवल देश वरन् समूचा विश्व चिन्तन और चरित्र की दृष्टि से गया गुजरा बन गया। वातावरण में दुष्प्रवृत्तियां भरीं तो अनेकानेक समस्यायें उलझी और विपत्तियां टूटी। इसे संभालने के लिए फिर सतयुग की वापसी की आवश्यकता है। यह कार्य साधु ब्राह्मणों की नई फसल नये सिरे से उगाने से होगा। इसकी पूर्ति युग अध्यात्म को ही करनी है और उसका शुभारम्भ प्रत्येक भावनाशील अध्यात्मवादी को अपने से ही प्रारंभ करना होगा।
जीवन को अध्यात्ममय बनाने के लिए आधा जीवन ब्राह्मण के रूप में और उत्तरार्द्ध साधु के रूप में व्यतीत करना चाहिए। घर में गुंजाइश न होने पर रोज कुंआ खोदने रोज पानी पीने जैसी स्थिति बन सकती है। तब सात घंटा सोने के लिए पांच घंटा नित्य कर्म हाट बाजार जैसे कामों के लिए और आठ घंटे कमाने के लिए यदि योजना बद्ध रूप से लगाये जायं, तो बीस घंटे में स्वार्थ प्रयोजन सधते रह सकते हैं और चार घंटे परमार्थ प्रयोजन के लिए मिल सकते हैं। इसमें से एक घंटा नित्य प्रज्ञा योग की साधना के लिए और शेष तीन घंटे जन सम्पर्क द्वारा लोक मानस परिष्कार के निमित्त लगाये जा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का पूर्वार्द्ध ब्राह्मण स्तर का बन सकता है। उत्तरार्द्ध को साधु परम्परा के अनुरूप पूरा समयदान लोक मंगल के लिए उत्सर्ग करना चाहिए। यही वानप्रस्थ धारण है। कुछ जमा पूंजी बच रही हो तो उसे बैंक में जमा करके उसके ब्याज से अपना गुजारा किया जाय या प्रज्ञा मिशन के माध्यम से अपने निर्वाह का प्रबंध किया जाय। घर-घर जाकर भिक्षा मांगने की पद्धति कभी उपयुक्त रही होगी; पर आज तो उसमें अपमान और कुधान्य की दोनों ही संभावनायें जुड़ गई हैं। अस्तु निर्वाह की दृष्टि से निश्चिन्त होकर अध्यात्म जीवन व्यतीत करने की योजना बनानी चाहिए। यह कार्य मात्र छुट-पुट पूजा पत्री मात्र से सम्पन्न नहीं हो सकता।
अध्यात्म तत्व ज्ञान और विधि विधान की शाश्वत रूप रेखा का स्वरूप स्पष्ट हो जाने पर उन भ्रान्तियों का निराकरण होना चाहिए जो आज इस क्षेत्र को तमसाच्छन्न किए हुए हैं। उसका कोई सत्परिणाम नहीं निकल रहा है। विडम्बनायें भर चल रही हैं। अंधी नकल हो रही है। धुनी जलाना वनवासी अध्यात्म प्रयोजनों के लिए इसलिए आवश्यक होता था कि वे शीत प्रधान हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। वहां वस्त्रों का, भोजन बनाने का, हिंस्र पशुओं को डराने का प्रयोजन पूरा होता था। जंगलों में ढेरों सूखी लकड़ी निरर्थक पड़ी रहती थी। उसे काम में लाने से वन प्रदेश की सफाई ही होती थी; पर आज तो स्थिति भिन्न है। लकड़ी कितनी महंगी है। वृक्ष कटने से उत्पन्न संकटों से सभी परिचित हैं। जो साधु सामान्य तापमान के क्षेत्रों में रहते हैं। वस्त्र भी पहनते हैं। हिंस्र पशुओं के आक्रमण का भय भी नहीं। फिर धूनी किसलिए जलाई जाय और उसके लिए निरन्तर इतनी राशि किसलिए गंवाई जाय?
वैज्ञानिक शोध कर्त्ताओं के लिए एकान्त वास आवश्यक होता है। विक्षेप न पड़े। प्राचीन काल में जो अध्यात्म क्षेत्र के मूर्धन्य शोध कार्यों में संलग्न होते थे। उन्हें अपनी काय प्रयोग शाला में अनेकों प्रकार के प्रयोग अनुसंधान अविष्कार करने होते थे। इस कार्य के लिए हिमालय जैसे क्षेत्रों में भवन बनाने की अपेक्षा प्रकृति विनिर्मित गुफायें ही उपयुक्त पड़ती थीं। उनमें रहकर वे अपना कार्य सुविधापूर्वक चला लेते थे। उपलब्धियों का लाभ जन साधारण तक पहुंचाना होता था तो प्रवास पर, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी प्रकार उनकी कार्य पद्धति का निश्चित रूप चलता रहता था। पर आज तो उसकी अन्धी नकल होती है। लोग शहरों के बीच तह खाने बनाकर उन्हें गुफा नाम देते हैं और उसमें पड़े-पड़े दिन गुजारते रहते हैं।
शरीर पर भस्म लगाने का प्रचलन इसीलिए था कि उसे लेपन से एक प्रकार की परत जम जाय और सर्दी गर्मी का प्रकोप शरीर को न सताये। किन्तु जिनके पास ढेरों कपड़े मौजूद हैं वे क्यों उस प्रकार का आडम्बर बनायें। क्षोर-कर्म की सुविधा न होने से बाल रखा लिए जाते थे। पर उनकी नकल करने के लिए नकली बालों का जटा जूट खरीद कर बालों में पिनों के सहारे सिर के बालों पर उसे क्यों लादे फिरा जाय? और क्यों लोगों को वास्तविकता रहित भ्रम में डाला जाय।
वनवासियों के लिए लौकी के या नारियल के कमंडलु हाथ से बना कर उससे पात्र का काम चलता रहता था। पर आज जब धातुओं के बर्तन बनने लगे हैं तो स्वच्छता और सुविधा की दृष्टि से उन्हीं का उपयोग किया जाय। चिमटा त्रिशूल, फरसा उन दिनों की उन क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक उपकरण रहे होंगे। उनसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बन पड़ती होगी पर आज तो उनका कोई प्रयोजन रह नहीं गया; फिर नाटकों के परिधान
बदल कर कुछ से कुछ बनने वाले नटों की कार्य पद्धति क्यों अपनाई जाय?
तीर्थ यात्रा का प्रयोजन धर्म प्रचार की पद यात्रा से था; पर उस कार्य पद्धति का परित्याग कर दिया गया तो बिना टिकिट यात्रा की चोरी करते हुए किस प्रकार का पुण्य अर्जित करने के लिए देवालय जलाशय देखते फिरते रहने के लिए क्यों समय का अपव्यय किया जाय?
अध्यात्म का वेष विन्यास या आडम्बर धारण की नकल बनाने की जरूरत नहीं है। पुरातन काल के आदर्शों और क्रिया कलापों को जब विस्मृत उपेक्षित कर दिया गया है तो उस प्रकार के वेष बनाने की विडम्बना रचने से क्या लाभ? दुकान में जो माल है ही नहीं उसकी बिक्री का साइनबोर्ड क्यों लगाया जाय? हमें अध्यात्म तत्व ज्ञान का उपहासास्पद आडम्बर नहीं बनाना है वरन् उस महान परम्परा को नये सिरे से पुनर्जीवित करना है।
स्वर्ग मुक्ति, सिद्धि, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर जो चलते हैं उन्हें अपने इन निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए निजी पुरुषार्थ से अपनी आजीविका चलानी चाहिए। सार्वजनिक धर पर आजीविका चलाने का अधिकार उन्हीं को है जो लोक मंगल के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। जिन्हें लौकिक या पारलौकिक स्वार्थ साधन करने हैं उनके लिए भिक्षा निर्वाह का, सार्वजनिक धन के उपयोग का कोई तुक रह नहीं जाता।