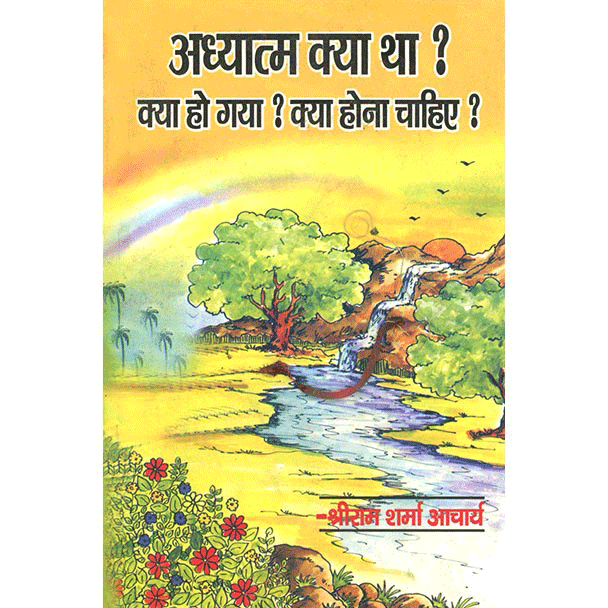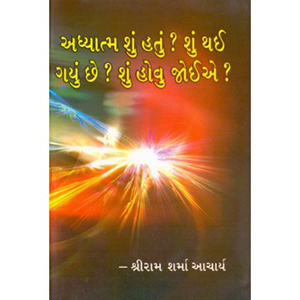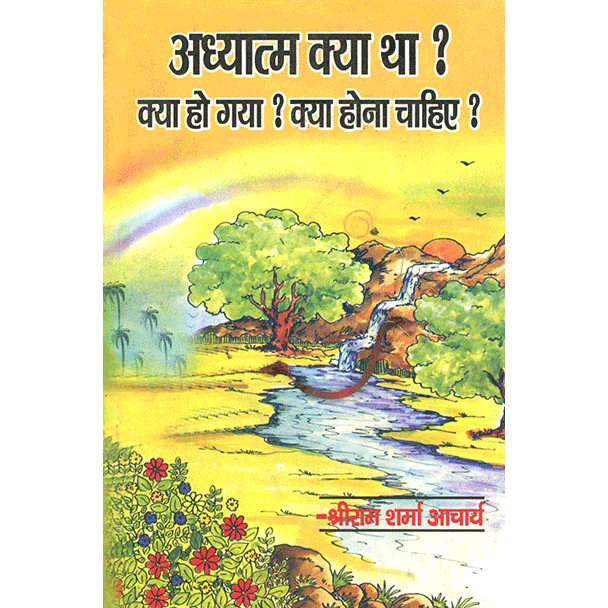अध्यात्म क्या था? क्या हो गया? क्या होना चाहिए? 
अध्यात्म में भ्रान्तियों का समावेश
Read Scan Versionअध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को उसकी वर्णमाला पढ़नी चाहिए और यह समझना चाहिए कि ब्रह्म चेतना का अवतरण किस आधार पर मनुष्य की सत्ता में प्रवेश करके उसे असाधारण रूप से शक्ति सम्पन्न बनाता है और वह अद्भुत कार्य कर दिखाने में क्यों कर समर्थ होता है? व्यक्ति के विकास और प्रतिभाओं-विभूतियों से सुसज्जित होने जैसी उसकी स्थिति क्यों कर बन पड़ती है?
परब्रह्म ब्रह्माण्डव्यापी चेतना शक्ति है। उनकी नियमन-व्यवस्था के अन्तर्गत ही समूचा सृष्टि क्रम चल रहा है। वह किसी से राग-द्वेष नहीं बनाती; मनुष्य की तरह अपने पराये का भेद-भाव भी उसके मन में नहीं होता न, उसे किसी की मनुहार चाहिए और न किसी का उपहार। जो समदर्शी और न्यायकारी है, उसके लिए किसी के साथ इस आधार पर लगाव नहीं हो सकता कि वह उसका बार-बार नाम रटता या अक्षत पुष्प चढ़ाता है।
प्रभु की अनुकम्पा किसी कारण विशेष से बरसती है और वहां जमा होती है, जहां उसे जमा होना चाहिए। गर्मी के बाद जब जल-थल सभी गरम हो उठते हैं, तब उसका संतुलन बिठाने के लिए वर्षा ऋतु आती है। पानी सर्वत्र बरसता है, पर वह जमा वहीं होता है, जहां निचाव है, गड्ढा या गहराई है। चट्टानों पर बरसने पर भी वह पानी वहां जमा नहीं हो पाता।
परब्रह्म के साथ जुड़ने और उसकी क्षमताओं-अनुकम्पाओं तथा विभूतियों को अपने पास तक बुलाने के लिए निजी-चुम्बकत्व चाहिए। चुम्बक अपने इर्द-गिर्द पड़े हुए लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है या स्वयं किसी बड़े चुम्बक की ओर खिंच जाता है। परमात्मा एक बड़ा चुम्बक है। हम उसकी ओर खिंच कर अपने में उन विशेषताओं को धारण कर सकते हैं, जो उसमें है।
जहां वृक्ष सघन होते हैं, वहां वर्षा भी खूब होती है। पेड़ों का आकर्षण बादलों को नीचे घसीटता है और उन्हें बरसने के लिए बाधित करता है। वर्षा का जल वहीं जमा होता है, जहां गहराई होती है। नदी-नाले तालाब इसीलिए जल से भरे रहते हैं कि उनमें गड्ढा होता है। हमें अपनी पात्रता विकसित करनी चाहिए, ताकि उसके अनुरूप परमात्मा का अनुग्रह और जन-समाज का सहयोग-सम्मान प्रचुर मात्रा में हस्तगत हो सके।
मानवी काया जादू की पिटारी है। उसके कण-कण में विलक्षण क्षमताओं के भंडार भरे पड़े हैं। नन्हें से परमाणु के अन्तराल में वही सारी गतिविधियां चलती हैं, जो बड़े रूप में सौर मण्डल के विशाल परिवार में चलती हैं, अन्तर इतना ही है कि वे प्रसुप्त और अदृश्य स्थिति में बीज रूप में अपने वैभव को छिपाये रहती हैं। इन्हें यदि सही ढंग से उभारा जा सके, तो पिण्ड रूप में दृष्टिगोचर होने वाला मनुष्य ब्रह्माण्डीय चेतना का प्रतिनिधि बन सकता है। मस्तिष्क के 7 प्रतिशत भाग का ही उपयोग जाना जा सका है, पर उसके 93 प्रतिशत उस भाग से अपरिचित ही हैं, जो अवचेतन-सुपरचेतन आदि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शरीर की नस-नाड़ियों में जो विद्युत प्रवाह बहता है, उसका एक बहुत थोड़ा अंश शरीर संचालन भर में काम आता है। कुछ बिजली सोचने-समझने भर में खर्च हो जाती है। उसका उच्चस्तरीय भाग, जो प्राण की प्रचण्ड शक्ति के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, उसका उपयोग नहीं के बराबर हो पाता है। कदाचित् इस प्राण-प्रखरता को जाग्रत, सशक्त और क्रियाशील बनाया जा सके, तो उतने भर से मनुष्य साधारण दीखते हुए भी असाधारण बन सकता है और महामानवों, ऋषियों, देवात्माओं की श्रेणी में बैठ सकने की स्थिति में अपने आप को समुन्नत कर सकता है। यह सफलता एवं उपलब्धि हस्तगत कर सकना पूर्णतया उसके हाथ की बात है।
मनुष्य की क्षमताएं, दोष-दुर्गुणों से, कषाय-कल्मषों से, कुकर्म और दुश्चिन्तन से दबी रहती है। अध्यात्म का पहला चरण यह है कि इन सब मलीनताओं से जूझें और उन्हें निरस्त करके रहें। इस प्रक्रिया को ‘‘तप’’ कहते हैं। तप का अर्थ है—अपने को तपाना। तपाने से तात्पर्य है अपनी बहिरंग और अंतरंग अनुपयुक्तताओं को तीक्ष्ण बुद्धि से खोज निकालना और उनके साथ जुड़े-बंधे स्वभाव और मन को ठोक-पीटकर सही करना। बाहर के शत्रुओं से लड़ना सरल पड़ता है, क्योंकि वे बाहर होते हैं और आंखों से दीखते हैं। उनके ऊपर कई साधनों से प्रहार या बचाव किये जा सकते हैं, पर अपने आप से कैसे जूझा जाय? दुष्प्रवृत्तियां स्वभाव का अंग बन कर अभ्यास में उतर जाती हैं और आदत बन कर इस प्रकार इसी काया में छिप जाती हैं कि उन्हें देख-समझ पाना तक कठिन पड़ता है। ऐसी दशा में कोई सूक्ष्मदर्शी ही उन्हें खोज सकता है और मित्र न मान कर शत्रु होने की मान्यता बदल सकता है। निपटने की रणनीति इसके उपरान्त ही बनती है।
गीता में अर्जुन को भगवान ने आनाकानी करने पर उसको जिस महायुद्ध में प्रवृत्त किया था, उसकी आध्यात्मिक व्याख्या अपनी सहचरी-कुटुम्बी बनकर रह रही अवांछनीयता के विरुद्ध प्रबल पराक्रम के साथ लड़ने में जुट पड़ने के रूप में ही हो सकती है। यह अनिवार्य युद्ध ही तप है। मात्र काय-कष्ट का अतिवाद अपनाने को तप नहीं कहते। इसके लिए अपने आप को धोबी की तरह कपड़े धोने में जो भट्टी चढ़ाने, साबुन लगाने, पीटने पछाड़ने जैसे काम करने पड़ते हैं, उन सभी का जुगाड़ बिठाना पड़ता है। तपस्वियों को यही रीति-नीति अपनानी पड़ती है।
तप के चार प्रधान आधार हैं—(1) इन्द्रिय संयम (2) समय संयम (3) अर्थ संयम (4) विचार संयम। इन चारों में ही जीवन बटा और बिखरा हुआ है। इन्हें कार्यान्वित करने में जीवन का प्रायः प्रत्येक पक्ष लपेट में आता है। इसलिए इस परिशोधन से एक प्रकार से समग्र जीवन का ही परिशोधन—परिष्कार करना पड़ता है। संकल्प और साहस के सहारे अभ्यास-आदतों से निपटना पड़ता है। मन की ललक लिप्साओं से स्पष्ट शब्दों में ‘नहीं’ कहना पड़ता है। कहना ही नहीं, वरन् दूरदर्शी विवेकशीलता को मूर्धन्य मान कर उसके आदेशों का परिपालन अनिवार्य हो सके, इसके लिए पुराने व्यक्तित्व को प्रशिक्षित करना पड़ता है।
आत्मशोधन एवं पात्रता संवर्धन के लिए जो दूसरा चरण उठाना पड़ता है वह है—‘‘योग’’। योग का शब्दार्थ जोड़ना होता है। जुड़ना किससे? परमात्मा से, परब्रह्म से। उसका एक ही उपाय है कि मानवी गरिमा के साथ जुड़ी हुई महानता को अपने जीवन क्रम में सम्मिलित करना। सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय ही मनुष्य का परमेश्वर है। उसके समग्र स्वरूप को तो अचिन्त्य ही कहा जा सकता है। मनुष्य का परमेश्वर क्या हो सकता है? उसे परमेश्वर न कह कर विराट्-ब्रह्म या विश्वब्रह्म ही कहना चाहिए, जीवनब्रह्म भी।
जीवन का योग इसी परमेश्वर के साथ हो सकता है। संक्षेप में इसे सत्प्रवृत्ति-संवर्धन भी कह सकते हैं। इस संबंध में वेदान्त दर्शन के सूत्र स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर देते हैं। सोऽहम्। शिवोऽहम्। सच्चिदानंदोऽहम्। तत्वमसि। अयमात्मा ब्रह्म, आदि शब्दों में जो रहस्य सन्निहित है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य का अन्तरंग और बहिरंग देवोपम होना चाहिए।
नर को नारायण—पुरुष को पुरुषोत्तम—अणु को विभु बनाने के लिए जो साधना करनी पड़ती है, उसके दो पक्ष हैं—प्रथम ‘तप’ द्वितीय ‘योग’ तप का तात्पर्य है—दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और योग का तात्पर्य है—सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। चिन्तन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता, और व्यवहार में शालीनता का समावेश जो जितनी मात्रा में कर सका, समझना चाहिए कि वह उसी स्तर की प्रगति आत्मोत्कर्ष में कर सका।
कपड़े को रंगने में पहले उसे धोना पड़ता है। खेत में बीज बोने से पहले उसे जोतना पड़ता है। दीवार खड़ी करने से पहले नींव खोदनी पड़ती है। देवता की स्थापना पूजा करने से पहले स्थान एवं उपकरणों को शुद्ध करना पड़ता है। तप परिमार्जन के लिए और योग परिष्कार के लिए होता है। जो इन दोनों प्रसंगों में अपने आपको सही सिद्ध कर लेता है, समझना चाहिए कि उसने उतना ही अपना पथ प्रशस्त कर लिया, परमलक्ष्य तक पहुंचने की उसकी तैयारी उसी मात्रा में पूरी हो गई।
माता बच्चे को प्राणों से अधिक प्यार करती है। उसकी सेवा सहायता में भी निरन्तर लगी रहती है, किन्तु जब वह कपड़ों में टट्टी कर लेता और अपने आपको उस गन्दगी में पूरी तरह सान लेता है, तो उसके आग्रह करने, मचलने पर भी माता न तो गोदी में लेती है और न दूध पिलाती है। उसका प्रथम प्रयास होता है—बच्चे को धोना, नहलाना, कपड़े बदलना। इतने कार्यों से जब शुद्धता पूरी हो जाती है, तभी वह उसे गोदी में उठाती, दूध पिलाती और खिलाती है। ईश्वर की रीति-नीति भी यही है। वह तब तक मनुष्य से खिंचा-खिंचा, असम्बद्ध रहता है, जब तक कि आत्म परिष्कार का प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता है। इस संदर्भ में बरती गई उपेक्षा ही वह स्थिति है, जिसके कारण उसे ईश्वर के विशिष्ट अनुदान प्राप्त करने में कठिनाई पड़ती है। आत्मशोधन ही वह कार्य है, जिसे सर्व प्रथम किया जाता है और उसके बाद आत्मिक प्रगति का परिष्कार का क्रम तेजी से चल पड़ता है।
परीक्षा-प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, उन्हें उत्तीर्ण किया जाता है। ऊंची श्रेणी हो, तो पुरस्कार भी दिया जाता है। किन्हीं ऊंचे पदों पर नियुक्ति होती है तो भी आवेदनकर्त्ताओं को प्रतियोगिता में बिठाया जाता है। जो उपयुक्त सिद्ध होते हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है। इसके उपरान्त भी कार्य कुशलता की समीक्षा होती रहती है और पदोन्नति का सुयोग बनता रहता है। यह कार्य बिना किसी पक्षपात के चलने का नियम है। लोकाचार में इसका व्यतिक्रम भी हो सकता है पर ईश्वर के दरबार में यह अकाट्य अनुबंध है। इसलिए ईश्वर की मनुहार करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी पात्रता उत्कृष्टता बढ़ाने के प्राणपण से प्रयत्न करें। आग पर तपाये जाने और कसौटी पर कसे जाने पर भी बार-बार खरे सोने की तरह अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते रहें। इसी आधार पर संसार में तथा परमात्मा के दरबार में किसी का मूल्यांकन होता है। इसी आधार पर किसी को दैवी अनुग्रह का अनुदान मिलता है। विभूतियां, ऋद्धियां, सिद्धियां हस्तगत होने का यह एक सुनिश्चित राजमार्ग है। पगडंडियों में भटकने वाले व्यर्थ ही भटकाव में पड़ते और अपने आपको कटीले जाल जंजाल में फंसाते हैं। उन्हें थकान, खीझ और निराशा ही हाथ लगती है।
संसार में कितने ही अन्धविश्वास फैले हुए हैं। लड़की-लड़के के बीच भेद-भाव करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। जातिगत ऊंच-नीच की मान्यता को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। नशेबाजी से किसका क्या भला हुआ है? शकुन मुहूर्तों की मान्यता कितने शंका संदेहों में उलझाती है, फिर भी लोग उन्हें मुद्दतों से माने चले जा रहे हैं। बौद्धिक भ्रान्तियों का पसारा भी कम नहीं है। उसने आधी दुनिया के चिन्तन को भ्रमित कर रखा है।
इसी प्रकार का एक भ्रम यह है कि ईश्वर को नामरट और पूजा पाठ से अपने वशवर्ती किया जा सकता है और उससे उचित अनुचित मनोकामनाओं को पूरा कराया जा सकता है। यह ईश्वर के शान में बहुत बड़े आक्षेप का आरोपण करना है, उसकी विवेक-बुद्धि को न्यायशीलता को कलंकित करना है। चारणों के मुंह प्रशंसा सुनकर जिस प्रकार मध्यकालीन सामन्त फूल कर कुप्पा हो जाते थे और उस यशगान के बदले उन्हें बहुमूल्य उपहार प्रदान किया करते थे, इसी स्तर का भगवान को मानें और उसे चापलूसी, चमचागिरी के आधार पर फुसलाने का प्रयत्न करें, तो समझना चाहिए कि ईश्वर की महानता को समझने में हम समर्थ नहीं हुए। भोग प्रसाद की, वस्त्र-छत्र चढ़ाने की रिश्वत देकर यदि हम उसके प्रिय पात्र बनना चाहते हैं और मनमर्जी से उचित-अनुचित काम कराना चाहते हैं, तो उसे धृष्टता ही कहा जायेगा। इस ओछे हथकंडों से हम किसी बैंक मैनेजर से मनचाही राशि प्राप्त नहीं कर सकते, परीक्षकों से भ्रष्ट कार्य नहीं करा सकते, न्यायाधीश को नहीं बरगला सकते और बिना योग्यता के ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होने का दांव चलाने में सफल नहीं हो सकते, तो फिर ईश्वर से उस प्रकार को ओछापन अपनाने की अपेक्षा किस आधार पर की जाय? वह इतना सूझबूझ रहित नहीं है, जिसे भजनानंदी लोग मछली या चिड़िया की तरह प्रलोभन देकर जाल में फंसा सकें और उसकी महानता को तलाक कर सकें।
साधना-उपासना का एकमात्र प्रयोजन आत्मशोधन और आत्मपरिष्कार है। एक शब्द में पात्रता अभिवर्धन है। कहा जा चुका है कि दुष्प्रवृत्तियों का निष्कासन ‘तप’ और सद्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन ‘योग’ है। इन आधारों को जो जितनी दृढ़ता और तत्परता के साथ अपनाता है, वह अपनी पात्रता बढ़ाते हुए परमेश्वर का प्राणप्रिय बनता है। चतुरता भरे हथकंडों को भक्ति नाम देकर उनके सहारे न ईश्वर का प्रियपात्र बन सकता है, और न उसके अनुग्रह से मिलने वाली विभूतियों का अधिकारी।
जप, ध्यान, पूजा, उपचार, कीर्तन, कर्मकाण्ड आदि का उद्देश्य यह है कि इन माध्यमों को अपना कर हम अपनी श्रेष्ठता और उदारता को अधिकाधिक विस्तृत और परिपक्व करें। इन उपचारों का रहस्य, संकेत समझते हुए उन कार्यों को करें, जो नियन्ता को अभीष्ट है।
मनुष्य जन्म को सुर दुर्लभ कहा गया है। स्रष्टा की यह सर्वोपरि आकृति है। इसे जीवन के हाथों इस आशा अपेक्षा के साथ धरोहर के रूप में सौंपा गया है कि निजी अपूर्णताओं को पूर्णता में विकसित किया जाय और साथ ही विश्व उद्यान को अधिकाधिक समुन्नत, सुविकसित बनाने की सेवा साधना में निरत रहा जाय। इस दूरदर्शी विवेकशीलता को व्यावहारिक जीवन में उतारने पर ही कोई सच्चे अर्थों में भक्त या साधन बन सकता है। संयम साधना से पुण्य सधता है और सेवा-साधना में निरत रहकर परमार्थ अर्जित किया जा सकता है। यह दोनों ही मिल कर उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिससे जीवन को सार्थक बनाने वाली गौरव-गरिमा हस्तगत होती है।
यदि अध्यात्म क्षेत्र में घुसे हुए भ्रम जंजाल से निकल कर उसके वास्तविक स्वरूप और क्रियान्वयन को समझा जा सके, तो उसका प्रतिफल निश्चित रूप से वही हो सकता है, जो शास्त्रकारों ने लिखा और आप्त पुरुषों ने कहा है। विज्ञान का पहला सिद्धान्त है कि किसी बात को सही तब माना जाय, जब प्रतिपादन के अनुरूप उसका प्रतिफल भी उपलब्ध हो सके। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने की बात सभी के गले उतरती है, इसलिए भौतिक विज्ञान ने मान्यता प्राप्त कर ली। अध्यात्म विज्ञान इस दृष्टि से पिछड़ा, फलतः अवज्ञा और उपेक्षा का भोजन बनने लगा है।