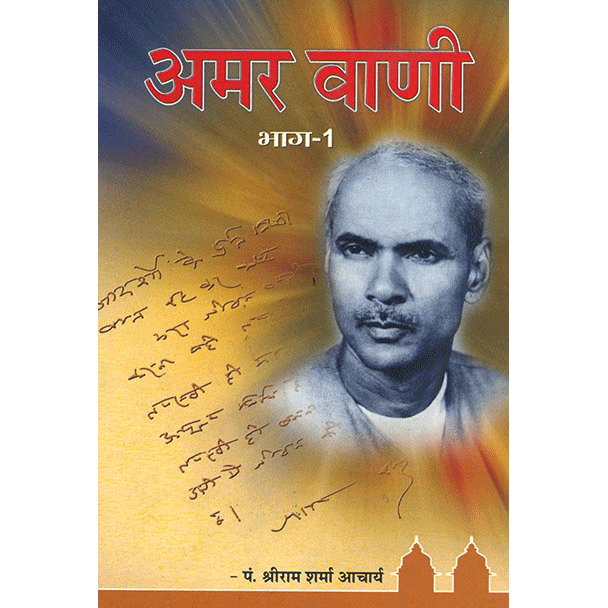अमर वाणी -2 
हमारा आत्मवादी जीवन दर्शन
Read Scan Versionमनुष्य को सदाचरण की मर्यादा में रखने, समाज के प्रति कर्त्तव्य पालन करने एवं स्नेह-सौजन्य का उदार परिचय देने के लिए तत्पर करना साधारण नहीं, असाधारण कार्य है। यह कार्य राजसत्ता के द्वारा किया तो जाता है, पर पूरी तरह सम्भव हो नहीं पाता। राजसत्ता का आयुध दण्ड है। कानून, पुलिस, कचहरी, जेल आदि तक उसका क्रियाकलाप सीमित है। इस पकड़ से बच निकलने के लिए मनुष्य हजारों रास्ते निकाल लेता है। अपराधियों में से थोड़े पकड़ में आते हैं। जो पकड़ जाते हैं, उनमें से बहुत कम को दण्ड मिलता है और जिन्हें दण्ड मिलता है उनमें से बहुत थोड़ों में सुधार होता है, अधिकांश तो उनमें से अपराधी प्रवृत्ति में पारंगत, अभ्यासी एवं निर्लज्ज ही हो जाते हैं। सुधार के उद्देश्य से बनाये गये प्रजातन्त्री कानून तो अपराधों के नियंत्रण में प्रायः असफल ही रहते हैं। यदि राजसत्ता ने कभी दुष्टता, दुर्बुद्धि को रोका है, तो उसके लिये नृशंस आतंकवादी दमन ही फलीभूत हुआ है।
आन्तरिक स्तर को उत्कृष्ट और समुन्नत बनाने के लिए दार्शनिक आस्थाएँ ही काम करती हैं। यह प्रयोजन धर्म, अध्यात्म और आस्तिकता के सहारे पूरा किया जाता रहा है। यह तत्त्वदर्शन यदि सही स्तर का हो, तो निस्संदेह उससे व्यक्ति की महत्ता को अक्षुण्ण बनाये रखने और विकसित करने का उद्देश्य पूरा होता रह सकता है। दुर्भाग्य यही रहा कि पिछले दिनों इन महान् अवलम्बनों को भी विकृत कर दिया गया। अब ईश्वर का रूप यह है कि वह थोड़ी पूजा-पत्री करने वालों से, भोग प्रसाद खिलाने वालों से प्रसन्न होकर पात्रता और पुरुषार्थ न होने पर भी मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाला मान लिया गया है। कर्मकाण्ड करने पर पाप कर्मों के दण्ड से छुटकारा मिलने की बात सरेआम कही जाती हैं, ऐसी दशा में आस्तिकवाद का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। भाग्यवादी परावलम्बन और पाप दण्ड से बचने की निर्भयता द्वारा व्यक्ति व समाज का पतन ही हो सकता है, उत्थान नहीं। अध्यात्म की विकृत मान्यताओं ने उसकी सारी उपयोगिता नष्ट कर दी।
दूसरा विकल्प देश-भक्ति, समाज निष्ठा नीति- शास्त्र के रूप में पिछले दिनों रखे गये हैं। पर वे दार्शनिक स्तर के नहीं रखे जा सके, उन्हें भौतिक उपयोगिता के आधार पर प्रतिपादित किया। फलतः नीति के रूप में उन्हें मान्यता मिली। आस्था के मर्मस्थल तक उनका प्रवेश न हो सका, यही कारण है कि समाज निष्ठा का जोर शोर से प्रतिपादन करने वाले लोग भी भीतर ही भीतर इतने कुकर्म करते पाये जाते हैं कि कथनी और करनी का भारी अन्तर आश्चर्यचकित कर देता है।
ऐसी दशा में परिष्कृत जीवन दर्शन का स्वरूप स्थिर करने की आवश्यकता सामने आती है। इसके लिए आत्मवादी वेदान्त दर्शन ही मन के उपयुक्त बैठता है। हम मूलतः ईश्वर के पुत्र राजकुमार और दिव्य विशेषताओं से भरे पूरे हैं। हमारे सामने ईश्वर द्वारा सौंपा गया आत्मपरिष्कार एवं लोक-मंगल का विशाल उत्तरदायित्व प्रस्तुत है। निकृष्ट चिन्तन एवं घृणित कर्तृत्व हमारी गौरव गरिमा पर लगा हुआ कलंक है, जिसे अविलम्ब निरस्त किया जाना चाहिए। यह विश्व भगवान् का साकार रूप है। इसे सुन्दर, सुव्यवस्थित, समुन्नत बनाने की कर्मठ साधना की जानी चाहिए। प्रत्येक के साथ सौहार्द्र, सौजन्य का व्यवहार किया जाना चाहिए। यही है आत्मवादी तत्त्वदर्शन, जिसे जन मानस में प्रतिष्ठापित करने के लिये युग निर्माण योजना द्वारा पूरी तत्परता के साथ प्रयुक्त किया जा रहा है। यदि यह आत्मवादी जीवन दर्शन लोक श्रद्धा में परिणत हो सका, तो विश्वास किया जाना चाहिए कि सतयुगी वातावरण का, मनुष्य कलेवर में देव ज्योति का दर्शन कर सकना निश्चित रूप से सम्भव हो सकेगा।
मनुष्य अपने आप में महान् है। उसमें सम्पूर्ण देव सत्ता और उत्कृष्टतम गरिमा ओत-प्रोत है। यह आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। माया, मलीनता, भ्रान्ति ही समस्त दुःख शोक का कारण है। इस मान्यता में आत्मानुभूति पर ही सारा ध्यान केन्द्रित किया गया है कि इस मार्ग पर जितनी प्रगति होगी व्यक्ति उतना ही महान् बनता चला जाएगा। यही आत्मदर्शन है। इसमें न ईश्वर भक्ति की तरह पक्षपात की आशा है और न समाज भक्ति की तरह बुद्धिबल के आधार पर उलटी-सीधी व्यवस्थाएँ गढ़ डालने की गुंजाइश। युग परिवर्तन का, भावनात्मक नवनिर्माण का आधार यह आत्मवाद ही हो सकता है। युग निर्माण परिवार के परिजनों को अपनी आस्थाएँ आत्मदर्शन के आधार पर विनिर्मित एवम् विकसित करनी चाहिए।
आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। हम अपनी मलीनताओं को तिलाञ्जलि देकर अधिकाधिक परिष्कृत और उदात्त बनें और अपूर्णताओं से विरत होकर पूर्णता का आनन्द लाभ करें, यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। इसमें किसी अन्य ईश्वर को, किसी अन्य आधार पर प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वरन् आत्मनिरीक्षण एवं आत्मशोधन पर ही ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। अन्तःकरण कितना उत्कृष्ट एवं उदात्त बना इसी कसौटी पर आत्मिक प्रगति की परख करनी पड़ती है।
हमें आत्मगौरव की रक्षा को परमात्मा के सम्मान की रक्षा के रूप में देखना चाहिए और आन्तरिक गरिमा पर आँच न आने देकर अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। ऊँचा उठने के लिए ऊँचे आदर्श अपनाने पड़ते हैं। हमारी भावनाएँ आत्मा के, परमात्मा के गौरव को सुरक्षित एवं सुविकसित रखने के लिए सब कुछ कर गुजरने की निष्ठा के साथ सुसम्बद्ध रहनी चाहिए।हम कोई ऐसा काम न करें जिसमें अपनी अन्तरात्मा ही अपने को धिक्कारे। इस तथ्य का निरन्तर ध्यान बनाये रखा जाए। अपनी क्षमताएँ और दुष्टताएँ दूसरों से छिपाकर रखी जा सकती हंै, दूसरों को झुठलाया और भ्रमाया जा सकता है, पर अपने आप से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। दूसरे तो किसी भी भय या प्रलोभन से अपने दोषों को सहन कर सकते हैं। पर आत्मा तो वैसा क्यों करेगा? आत्म-धिक्कार, आत्म-प्रताड़ना, आत्म-असन्तोष, आत्म विद्रोह मानवी-चेतना को मिलने वाला सबसे बड़ा दण्ड है। शरीर को दर्द, चोट, ताप आदि से कष्ट होता है। मन को शोक, अपमान, घाटा, विछोह आदि से दुःख होता है। पर आत्मा को तिलमिला देने वाली पीड़ा तो आत्मधिक्कार के रूप में ही सहनी पड़ती है।
अपना कर्त्तव्य, अपना चिन्तन, अपना स्तर-अपनी ही आत्मा के सामने तो स्पष्ट रहता है। उससे कुछ कैसे छिप सकता है? फिर यह भी स्पष्ट है कि शुद्ध, बुद्ध और निरञ्जन ईश्वर का प्रतीक प्रतिनिधि होने के कारण वह निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका ही सम्पन्न करता है और अनाचार को सहन न करके आत्मधिक्कार की प्रचण्ड प्रताड़ना से सारा व्यक्तित्व हिल जाता है और मनुष्य हर घड़ी बेतरह काँपता रहता है। इस कँपकँपी की प्रतिक्रियाएँ शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक स्तर में अगणित उद्वेग बनकर सामने आती हैं। मनुष्य को कहीं चैन नहीं मिलता। हर घड़ी उचटा-उचटा, उद्विग्न और अशान्त रहता है। साधन कितने ही अधिक क्यों न हों। लगता है उसका कुछ छिन गया, कुछ खो गया, कुछ भूल गया, कहीं भटक गया और किसी भारी विपत्ति के जंजाल में वह फँस गया।
बाहर से इस अशान्ति का कोई कारण नहीं दीखता पर भीतर की बेचैनी, अविश्रान्ति इतना उद्वेग उत्पन्न करती है, मानो किसी ने लगातार भगाया, दौड़ाया हो, मुद्दतों से सोने का अवसर न मिला हो। अगणित शारीरिक और मानसिक रोग इस आत्मधिक्कार की प्रताड़ना से ही उत्पन्न होते हैं। इस आत्मदण्ड से पीड़ित व्यक्ति प्रचुर साधन सम्पन्न होते हुए भी निरन्तर व्याकुल-बेचैन रहता है।
मरने के बाद स्वर्ग-नरक मिलने, न मिलने की बात पर सन्देह किया जा सकता है, पर घृणित जीवनक्रम अपनाये हुए व्यक्ति की आत्मप्रताड़ना को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और उसकी प्रतिक्रिया कितने उद्वेग, अवरोध बनकर सामने खड़ी होती है, इसको कभी भी, कहीं भी, अनुभव किया जा सकता है। यह नरक जीवित स्थिति में ही हर घड़ी भुगतना पड़ता है। अपना आपा ही आदमी को इतना डरावना लगता है, मानो हजार यमदूतों का प्रतीक बनकर वह असंख्य नरकों को ऊपर उलीचने के लिए आतुर खड़ा हो।
आत्मदर्शन इन्हीं तथ्यों की ओर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है और इंगित करता है कि छोटे-छोटे इन्द्रियलिप्सा जन्य लोभ, मोह के आकर्षणों से प्रेरित, अवांछनीय गतिविधियों से बचा ही जाना चाहिए। अहंताजन्य ईर्ष्या और एषणाओं के लिए व्याकुल नहीं रहना चाहिए। अपनी आँख में अपना सम्मान जिससे बढ़ सके, अन्तःकरण में निवास करने वाला परमात्मा जिससे सन्तुष्ट और सहमत हो सके, ऐसे ही क्रियाकलाप अपनाने चाहिए, ऐसा ही दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। आत्म-दर्शन को यदि सचमुच अपनाया गया होगा, तो आत्मशोधन और आत्मपरिष्कार की प्रबल उत्कण्ठा अन्तःकरण में उठ खड़ी होगी। उसे किसी भी कारण से अवरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।
आत्मगौरव की माँग है कि शानदार जीवन जिया जाय। शानदार सोचा और शानदार किया जाय। देश की आन-बान, शान पर सब कुछ निछावर करने वाले स्वाभिमानी, सेनानायकों से कम नहीं, वरन् बढ़कर आत्मवादी होता है। उसको आत्मा की, परमात्मा की, शान की चिन्ता रहती है। इसकी इज्जत बनाए रखने के लिए उसे बड़ा त्याग करने में हिचक नहीं होती।
आत्मवादी न दुष्ट हो सकता है न कुकर्मी। न छल कर सकता है, न प्रपञ्च रच सकता है। निकृष्ट चिन्तन से भी उसे घोर घृणा होती है। मस्तिष्क भगवान् विष्णु का क्षीर सागर, शिव का कैलाश, मानसरोवर और ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है। ऐसे पवित्र स्थान में पिशाच और चाण्डाल जैसे दुष्ट-दुर्भावों का क्या काम? अनैतिक और पतनोन्मुख विचारों को ऐसे देव स्थान में गन्दगी बिखेरने का अवसर कैसे दिया जा सकता है? आत्मभाव की भूमिका में जीवित मनुष्य इस दिशा में पूर्णतया सजग और सतर्क रहता है।
व्यक्तिगत जीवन में जिस उच्चस्तरीय ‘शुचिता’ का समावेश भावनात्मक नव-निर्माण में प्रधान रूप में रचा गया है, उसकी स्थापना पुष्टि और परिपक्वता आत्मदर्शन की प्रौढ़ता के साथ जुड़ी है। हममें से प्रत्येक को आत्म-गौरव की, आत्मसम्मान की, आत्म-परिष्कार की, आत्म साक्षात्कार की चेष्टा करनी चाहिए। आत्मसम्मान के नाम पर कई बार ओछे स्तर का अहंकार विदूषक जैसा वेष बनाकर सामने आ खड़ा होता है। हमारा अहंकार वस्तुओं और परिस्थितियों को खोजता है और उनके आधार पर रुष्ट, तुष्ट होता है, जबकि आत्म-गौरव आन्तरिक स्तर पर-गुण, कर्म, स्वभाव के स्वरूप पर, आकांक्षाओं और विचारणाओं की दिशा पर आधारित रहता है। जिसकी अन्तःभूमिका उज्ज्वल है उसे बाह्य परिस्थितियों से कुछ लेना-देना नहीं रह जाता। उसे भौतिक जीवन की सफलता, असफलताएँ प्रभावित नहीं करती। सम्पदाएँ नहीं आन्तरिक विभूतियाँ उसकी सन्तुष्टि का केन्द्र रहती हैं। अहंकारी व्यक्ति जहाँ बाह्य प्रतिकूलताएँ देखकर ही असन्तुलित और रुष्ट-असन्तुष्ट होने लगता है, वहाँ आत्मवादी को आन्तरिक स्तर की उत्कृष्टता ही परिपूर्ण सन्तोष दे सकने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है।
आत्मवादी अपने शरीर, मन और व्यवहार को ऐसा उज्ज्वल, उत्कृष्ट बनाने में लगा रहता है, जिससे इस कायकलेवर में निवास करने वाले आत्मा का गौरव बढ़ता हो। शरीर स्वच्छ, वस्त्र स्वच्छ, उपकरण स्वच्छ, घर स्वच्छ, उसका निवास और प्रभाव जहाँ भी रहेगा, वहाँ स्वच्छता की प्रतिष्ठापना के लिए निरन्तर प्रयास चल रहा होगा। आन्तरिक स्वच्छता जहाँ होगी, वहाँ बाह्य स्वच्छता भी छाया की तरह साथ रहेगी। गन्दगी से जुड़े रहना मनुष्य के स्तर पर लगने वाली लाँछना है। इसे कोई स्वाभिमानी क्यों सहन करेगा?
सृष्टि का हर काम पूर्ण व्यवस्था और क्रमबद्धता के साथ चल रहा है। सूर्य नियत समय पर उगता-डूबता है। मनुष्य की दिनचर्या नियमित और नियन्त्रित होनी चाहिए। उसे एक क्षण भी अस्त-व्यस्त स्थिति में नहीं गुजारना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त सबसे प्रधान सम्पदा के रूप में जीवन के क्षण ही तो मिले हैं, इनमें से एक क्षण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। समय का पूरा-पूरा सदुपयोग किया जाना चाहिए। अस्त-व्यस्तता के लिए, आलस्य, प्रमाद के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हर काम क्रमबद्ध, योजनाबद्ध, व्यवस्थित और कलात्मक, सम्पूर्ण मनोयोग के साथ किया हुआ होना चाहिए। आत्मवाद की मान्यता कहाँ कितनी गहरी है, इसे किसी की कार्यपद्धति में सतर्कता और सजगता के समावेश के रूप में देखा-परखा जा सकता है। उसमें आलस्य, प्रमाद के लिए, लापरवाही और उपेक्षा के लिए कहीं रत्ती भर भी गुंजाइश न मिलेगी।
हर किसी से मधुर भाषण, नम्र व्यवहार, शिष्टता और शालीनता का समुचित समावेश, हर किसी का आदर, चेहरे पर सन्तोष और उल्लास व्यक्त करती रहने वाली अनवरत एवं अभ्यस्त हल्की मुसकान को देखकर यह जाना जा सकता है कि आत्मवाद का रंग कितना गहरा चढ़ा है। सज्जनता, सादगी और संजीदगी की मात्रा के अनुरूप किसी के अन्तःकरण का स्तर गिरा या उठा हुआ नापा जा सकता है। विरोध और मतभेद में भी अनौचित्य के साथ ही लड़ाई को सीमित रखने की, व्यक्ति के नाते हर किसी का सम्मान करने की कला जिसे आ गई, समझना चाहिए अपनी और दूसरों की आत्मा के सम्मान सुविधा की आवश्यकता का तथ्य जान लिया गया।
आत्मगौरव और कर्त्तव्यनिष्ठा परस्पर अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मनुष्य के कन्धे पर अनेक कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व रखे गए हैं। नागरिक कर्त्तव्यों का पालन हर किसी के लिए आवश्यक है। स्त्री, बच्चे, माँ-बाप, भाई-बहिन, मित्र, पड़ोसी, सेवक, स्वामी सभी के प्रति अपने कुछ कर्त्तव्य हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं। इन सबको सही ढंग से निबाहने पर ही आत्मगौरव की रक्षा हो सकती है। मर्यादाओं का पालन किया ही जाना चाहिए। पशु प्रवृत्तियों और कुसंस्कारों पर नियन्त्रण रखना ही चाहिए। अधिकारों के लिए उतना बेचैन नहीं होना चाहिए जितना कि कर्त्तव्य पालन में भूल न होने देने के लिए। दूसरे लोग क्या करते हैं? उनने क्या बदला चुकाया और लेखा-जोखा लेने की अपेक्षा इतना सोचना ही पर्याप्त है कि हमने अपना कर्त्तव्य पूरा किया या नहीं? दूसरे भूल करते हैं तो उनसे अपनी तुलना क्या? आत्मवादी को आदर्श बनना पड़ता है, ताकि दूसरों को अनुकरण का उदाहरण और सन्मार्ग पर चलने का प्रकाश अवलम्बन, आधार मिल सके।
आत्मवादी हराम की, अनीति की कमाई नहीं खा सकता। पाप का पैसा खाने से भूखा मरना अच्छा। यह सिद्धान्त जिसने अपना लिया वह न्यायोचित उपलब्धियों में ही गुजारा करने की व्यवस्था बनाता है, दुनिया में बहुत लोग गरीबी का जीवन जीते हैं। रूखा-सूखा खाकर, फटा-टूटा पहनकर ईमानदारी का जीवन जीने में आत्मवादी की शान है। वह बेईमानी की, हराम की, चोरी, चालाकी की कमाई की ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखता। न उसे जुआ खेलना आता है, न सट्टा-लाटरी लगाने को मन चलता है। बीसों उँगलियों की-पूरे परिश्रम की, खरी कमाई खाकर जिस स्तर का भी रहन-सहन रखा जा सके, वह उतने में ही बादशाहों जैसी शान समझता है। उचक्के लोग अय्याशी का ठाठ-बाट बनाए फिरते हैं, उससे उसे न ईर्ष्या होती है, न इच्छा। ईमानदारी की कमाई अपने आप में इतनी शानदार है कि उसके लिए चने चबाकर और टाट ओढ़कर जीना पड़े, तो उसे अपने लिए शान और सम्मान भरा उपहार ही मानना चाहिए।
आत्मनिष्ठ का जीवन उसकी निष्ठा का सूचना पट होता है। बेईमानी की कमाई से जो वैभव प्रदर्शन किया जाता है, वह एक तरह से अपनी अनैतिकता की सार्वजनिक घोषणा है। कोई सुप्तात्मा ही अपने बेईमान होने के इस सूचना पट को लगाकर प्रसन्न हो सकता है। आत्मवादी इसके लिए ललचाना तो दूर, उस ओर फूटी आँख देखना भी पसन्द न करेगा। उसे तो आत्मा का वर्चस्व बढ़ाने वाली हर क्रिया रुचिकर लगेगी। न वह भौतिकता की आकांक्षा करेगा और न उससे प्रभावित होगा। उसे कुछ प्राप्त भी हो जायेगा, तो किसी आवश्यकता युक्त व्यक्ति की ओर ही उसे बढ़ा देगा।
आत्मवाद की प्रेरणा है, आत्मगौरव की रक्षा। कहना न होगा कि आत्मगौरव, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा, सज्जनता और सुव्यवस्था से भरे जीवनक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा ही जीवनक्रम स्वयं अपनाना चाहिए और ऐसी ही आस्था अपने परिवार प्रभाव क्षेत्र में उत्पन्न करनी चाहिए।
-वाङ्मय-६६,१.२०-२३
यदि विचार बदल जाएँगें तो कार्यों का बदलना सुनिश्चित है। कार्य बदलने पर भी विचारों का न बदलना सम्भव है, पर विचार बदल जाने पर उनसे विपरीत कार्य देर तक नहीं होते रह सकते। विचार बीज हैं, कार्य अंकुर, विचार पिता हैं, कार्य पुत्र। इसलिए जीवन परिवर्तन का कार्य विचार परिवर्तन से आरंभ होता है। जीवन-निर्माण का, आत्म-निर्माण का अर्थ है-‘विचार-निर्माण।’
-वाङ्मय-६६,२.१९
Write Your Comments Here:
- भविष्य इस प्रकार उभरेगा
- सूर्योदय हो चला अब प्रकाश फैलाना ही बाकी है
- सतयुग की वापसी
- भारत का भविष्य निश्चित रूप में उज्ज्वल है
- आन्तरिक्ष में चल रही उच्चस्तरीय उथलपुलें
- विनाश विभीषिकाओं का अन्त होकर रहेगा
- प्रतिभायें अग्रिम पंक्तियों में आये
- युग परिवर्तन-नियन्ता का सुनिश्चित आश्वासन
- परिवर्तन की अदृश्य किन्तु अद्भुत प्रक्रिया
- निकट भविष्य में यह परिस्थितियाँ सामने आयेंगी
- हमारा आत्मवादी जीवन दर्शन
- इस अभियान के साधन यों जुटेंगे
- परिवार जीवन विकास की प्रयोगशाला
- युग निर्माण परिवार के सदस्य इस भाँति सोचें