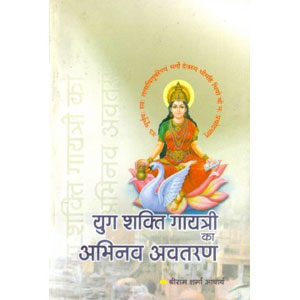युगशक्ति गायत्री का अभिनव अवतरण 
व्यक्तित्व के विकास में, गायत्री साधना का उपयोग
Read Scan Version
गायत्री उपासना का दर्शन और विधान व्यक्तित्व के समग्र विकास की आवश्यकता पूरी करता है। इस प्रक्रिया में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है। इस उपक्रम को अपनाने वाला उपासना की अवधि में अपने चिन्तन को उच्च स्तर का बनाता है और शरीर को ऐसे क्रिया कृत्यों में लगाता है जिनसे आदर्शवादिता की ओर अग्रसर होने की भाव भरी प्रेरणा मिलती है।
न तो मात्र चिन्तन ही पूर्ण है न अकेला कर्म ही। दोनों का प्रथक-प्रथक अस्तित्व तो है और उनसे यत्किंचित् प्रतिफल भी प्राप्त होता है, पर वह रहता सर्वथा अपूर्ण एवं एकांगी ही है। बिजली के दोनों तार मिल कर ही प्रवाह पैदा करते हैं उसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सत्परिणाम उत्पन्न करता है। गायत्री उपासना में उत्कृष्ट जीवन के लिये अभीष्ट ज्ञान और कर्म का इस प्रकार समन्वय है कि उसे व्यक्तित्व के विकास का ऐसा समग्र शिक्षण कह सकते हैं जिसमें चिन्तन और कर्मकाण्ड का उपयुक्त सन्तुलन बहुत ही दूरदर्शिता के साथ मिलाकर रखा गया है।
उपासना काल में साधक का चिन्तन सर्वथा अन्तर्मुखी रहता है। बाहरी संसार का विचार और कर्म करते-करते ही पूरा समय बीतता है। पूजा पर्व का थोड़ा-सा समय इसके लिए सुरक्षित रखा गया है कि उस अवधि में मात्र अन्तर्मुखी चिन्तन किया जाय और अन्तर्जगत में सम्बन्धित तथ्यों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाय। जब तक इसी प्रयोजन में मन लगा रहता है तब तक साधना में मन लगा समझा जाता है। सन्तोष मिलता है और सत्परिणाम भी मिलता है किन्तु यदि मन थोड़े से समय में भी भौतिक जीवन का—वाह्य संसार का ही चिन्तन करने के लिये दौड़ता रहे तो समझना चाहिए साधना अधूरी रह गई। मनोनिग्रह की आवश्यकता इसी लिए समझी जाती है कि उस अवधि में जो कुछ सोचा और किया जाय वह आत्मिक क्षेत्र से ही सम्बन्धित हो। जितनी देर ऐसा बन पड़ता है समझा जाता है कि उपासना का उपक्रम ठीक तरह बन पड़ा। उपासना का पूर्वार्ध (1) स्वाध्याय (2) सत्संग (3) चिन्तन (4) मनन है। इनमें आत्म-समीक्षा, आत्म-सुधार, आत्म-निर्माण और आत्म-विकास के सन्दर्भ में विभिन्न समस्याओं का स्वरूप एवं समाधान समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसे साधना का तत्वज्ञान एवं दर्शन पक्ष कह सकते हैं। ब्रह्म-विद्या का सारा कलेवर इस प्रशिक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही खड़ा किया गया है। कथा, प्रवचनों का यही उद्देश्य है।
उपासना का उत्तरार्ध वह है जिसे कर्मकाण्ड उपचार के साथ सम्पन्न किया जाता है। इसके भी चार चरण हैं—(1) पवित्रीकरण (2) देव पूजन (3) जप (4) ध्यान। प्रायः इन्हीं चार वर्गों में ही साधना विधि-विधान आ जाता है। रुचि भिन्नता और परिस्थिति विशेष के कारण विभिन्न प्रकार के साधन विधान बनते रहे हैं। पर उन सबको यदि वर्गीकृत करना हो तो चार में उन सबका समावेश हो सकता है।
पवित्रीकरण में पवित्र नदी सरोवरों का स्नान, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, उपकरण शुद्धि आदि सम्मिलित हैं। पूजा उपचार आरम्भ करने से पहले आत्म शोधन के लिए मार्जन, आचमन, प्राणायाम, न्यास, अघमर्षण आदि की क्रियाएं सम्पन्न करनी पड़ती हैं। देव पूजन में प्रतिमा पूजन, षोडशोपचार, स्तवन, अभिषेक, आरती, परिक्रमा, मन्दिर दर्शन, सूर्यार्घदान, कलश स्थापना, दीप स्थापन, हवन आदि कृत्यों को गिना जा सकता है।
जप में मन्त्रों के रूप में जाने, जाने वाले शब्द गुच्छकों की रटन, पुनरावृत्ति, कीर्तन, मानसिक जप, सोहम् का अजपा जप, अखण्ड पारायण, ग्रन्थ पाठ आदि की गणना होती है।
ध्यान में बिन्दु योग, लययोग, नादयोग, चक्रवेधन, पंचकोश साधना, प्राणयोग, ऋणयोग, विन्दुयोग आदि वे सभी साधनाएं आ जाती हैं जिनमें चिन्तन को एक विशिष्ट दिशा धारा में प्रवाहित करना पड़ता है।
इस प्रकार समग्रयोग के आठ अंग हैं। भगवती साधना में दुर्गा की आठ भुजाओं के रूप में शास्त्रकारों ने इन्हीं का निरूपण किया है।
देखना यह है कि इन आठों क्रिया कृत्यों से किस प्रकार व्यक्तित्व का निखार और उभार सम्भव होता है। मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए इन विधि-विधानों का किस प्रकार—किस मर्मस्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्य दृष्टि से यह सभी उपचार जादुई लगते हैं और प्रतीत होता है कि इनमें कोई रहस्यमय प्रक्रिया भरी होगी, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। साधना विधियों को प्रतीक पूजा कहा गया है। इनके क्रिया कृत्यों में चिन्तन और कर्तृत्व में उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ने की भाव भरी प्रेरणाओं का समावेश है। इन प्रेरणाओं को जितना व्यावहारिक जीवन में उतारा जाता है, उसी अनुपात से अन्तर की दिव्य शक्तियां उभरती हैं और उस उभार के अनुरूप, सिद्धियां और विभूतियों के चमत्कारी प्रतिफल सामने आते हैं।
पवित्रीकरण के अन्तर्गत जल सिंचन, तीन आचमन, न्यास, अघमर्षण प्राणायाम आते हैं इनमें जल, वायु एवं अंग स्पर्श के माध्यम से अन्तरंग और बहिरंग की पवित्रता धारण करने के निर्देश हैं। शारीरिक कषाय और मानसिक कल्मष ही आत्मिक प्रगति के प्रमुख अवरोध हैं। उन्हें हटाने, समग्र स्वच्छता अपनाने से अन्तरात्मा में भगवान की अनुकम्पा एवं दिव्य समर्थता का अवतरण सम्भव होता है। यह तथ्य समझाने और अपनाने के लिए पवित्रीकरण के पांचों उपचार हैं।
दूसरा उपचार देव पूजन है। दूसरा तात्पर्य है देवत्व की गरिमा को स्वीकार करना और उसके सम्मुख नतमस्तक होना-पक्षधर बनना। आमतौर से सामान्य जीवन दैत्य उपासक ही रहता है। दैत्य अर्थात् वैभव, सुविधा साधन, लिप्सा-लालसा का तुष्टीकरण। इन्हीं कुचक्र में सारा श्रम और मनोयोग खप जाता है। देवत्व की कल्पना भर भले ही होती रहे, पर उसके परिपोषण के लिए कुछ बच ही नहीं पाता। इस पशु प्रवृत्ति को उलटने का संकल्प ही देव पूजन है। देवता की प्रतिमाओं के पीछे आदर्श भरे पड़े हैं। प्रतिमाएं एक प्रकार की पुस्तकें हैं जिनकी आकृतियों और प्रकृतियों के समुच्चय से यही बताया गया है कि देवानुयायी का चरित्र और चिन्तन कैसा होना चाहिए। देव पूजन में जो उपचार वस्तुएं काम आती हैं वे भी सद्गुणों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें अपनाने वाले पर देव कृपा बरसने का तथ्य प्रकट करती हैं। जल अर्थात् पवित्रता-तरलता। पुष्प अर्थात् कोमलता सुषमा। चन्दन अर्थात् उदारता, श्रद्धा। दीपक अर्थात् परमार्थ परायणता, प्रकाश प्रज्ञा। नैवेद्य अर्थात् मधुरता, अंशदान निष्ठा। अर्घ्यदान-श्रेष्ठता के प्रति समर्पण-विसर्जन। देवता के सम्मुख इन उपचारों को पूजा उपकरण के रूप में प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इन सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की अनिवार्य शर्त है जिसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्न किये ही जाने चाहिए।
जप का तात्पर्य है—अनवरत और अथक प्रयास एवं अभ्यास की निरन्तर पुनरावृत्ति। आमतौर से एक काम पर से मनुष्य का मन जल्दी ही ऊब जाता है और नवीनता की तलाश होने लगती है। चंचलता की यह वानर वृत्ति महान कार्यों के लिए आवश्यक अध्यवसाय बनने ही नहीं देती। उच्चस्तरीय कार्यों में बाल-क्रीड़ा जैसा कौतुक भी नहीं होता वे साधारण मनःस्थिति को नीरस ही लगते हैं। इसलिए क्षमता सम्पन्न व्यक्ति भी कोई महत्वपूर्ण कार्य—निरन्तर अध्यवसाय न अपना सकने के कारण कर नहीं पाते। आरम्भ भी करें तो मन की ऊब वैसा करने नहीं देती। इस मोर्चे को वही जीत सकता है जिसने मन जीता हो। कहते हैं कि जो अपने को जीतता है वही दूसरों को—संसार को—जीत पाता है। यहां मनोजप की ही चर्चा है। इसका अभ्यास जप के माध्यम से भली प्रकार हो सकता है। एक ही रटन को धैर्यपूर्वक देर तक करते रहने से नवीनता की तलाश के लिए उचक-मचक करने वाली वानर वृत्ति पर अंकुश लगता है और वह प्रवृत्ति जगती है जिसके अनुरूप नीरस दीखने वाले महान कार्यों पर धैर्यपूर्वक चित्त-वृत्तियों को जमाये रहा जा सके। यह चित्त-वृत्तियों का निरोध ही महर्षि पातंजलि के अनुसार योग है। योग साधना का प्रथम चरण जप माना गया है उससे शरीर और मन दोनों को धैर्यपूर्वक अनवरत क्रम से एक ही कार्य को करते रहने का स्वभाव बनता है। महत्वपूर्ण कार्य कर सकने के लिए यह अभ्यास नितान्त आवश्यक है।
जप के उपरान्त दूसरा चरण है ध्यान। शारीरिक गतिविधियों को जप के द्वारा अध्यवसाय रत रहने के लिए प्रशिक्षित अभ्यस्त किया जाता है। इसका अगला चरण है मन-मस्तिष्क। चिन्तन को एक केन्द्र पर नियोजित किये रहना—एक दिशाधारा में संलग्न रहना—यही है ध्यान धारणा का उद्देश्य। मन में कितनी प्रचण्ड शक्ति भरी पड़ी है किन्तु वह बिखराव से ही अस्त-व्यस्त और नष्ट-भ्रष्ट होती रहती हैं। यदि एकाग्रता पा सके तो सामान्य स्तर का मनुष्य भी विद्याध्ययन अनुभव सम्पादन—शोध कार्य—विशिष्ट कला-कौशलों का उपार्जन जैसी चमत्कारी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। एकाग्रता साधने वाले व्यक्ति ही वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, योग निष्णात होते देखे गये हैं। सांसारिक प्रयोजनों में भी महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने में एकाग्रता के अभ्यास की ही प्रधान भूमिका रहती है।
अन्तर्जगत की विभूतियां वाह्य जगत की सम्पदाओं से भी अधिक मूल्यवान हैं। समष्टिगत भौतिक सम्पदाएं जल, थल और आकाश में से निकालनी होती हैं। किन्तु व्यक्ति को विभूतिवान बना सकने के लिए जिन दिव्य उपलब्धियों की आवश्यकता होती है उन्हें अपने भीतर ही खोजा जा सकता है। दृष्टिकोण, मान्यताएं, आस्थाएं, इच्छाएं, आदतें, उमंगें, सम्वेदनाएं आदि की भाव सम्पदाएं ही मिलकर व्यक्तित्व को ढालती हैं और उसी आन्तरिक वैभव के आधार पर मनुष्य का वाह्य जीवन ढलता है। पिछड़ेपन और प्रगतिशीलता का उद्गम केन्द्र अन्तःक्षेत्र से ही प्रकट और प्रवाहित होता है। गढ़े खजाने की तरह मनुष्य जीवन की वास्तविक और बहुमूल्य सम्पदाएं उसके अन्तःक्षेत्र में ही भरी पड़ी हैं। इन्हें जानना, खोदना, उभारना और विकसित परिष्कृत करने का विज्ञान ही ध्यान योग है। ध्यान को अन्तर्जगत के अंधेरे में फेंकी जाने वाली सर्चलाइट कहा गया है। उस आधार पर उस दिव्य क्षेत्र की स्थिति को जानना और बिखरी पड़ी दिव्य सम्पदाओं को बटोर लाना सम्भव होता है।
आत्म-निरीक्षण, आत्म-सुधार, आत्म-निर्माण और आत्म-विकास का समुच्चय ही आत्मिक प्राप्ति है। उसी मार्ग पर चलते हुए अपूर्णता की पूर्णता में परिणिति और लक्ष्य प्राप्ति में सफलता सम्भव होती है। उस प्रसंग के सारे क्रिया-कलाप अन्तर्जगत में ही करने होते हैं और उनके लिए मानसिक एकाग्रता का प्रखर उपयोग ही कारगर सिद्ध होता है। ध्यान के द्वारा यही चेतनात्मक प्रखरता प्राप्त होती है और इसके द्वारा अन्तर्जगत में उपयोगी परिवर्तन परिष्कार कर सकना सम्भव होता है।
गायत्री उपासना का उत्तरार्ध आत्म-शोधन, देव-पूजन, जप और ध्यान है—इन चारों का उपयोग आत्म-निर्माण के लिए क्रिया योग के रूप में किया जाता है। उसे पूर्वार्ध का—स्वाध्याय सत्संग—मनन-चिन्तन का पूरक ही माना जाना चाहिए। व्यक्तित्व के समग्र विकास को ही भौतिक और आत्मिक सम्पदाओं का—ऋद्धि-सिद्धियों का केन्द्र माना गया है। उस प्रयोजन की पूर्ति में गायत्री उपासना का तत्वज्ञान और विधि-विधान असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है।
न तो मात्र चिन्तन ही पूर्ण है न अकेला कर्म ही। दोनों का प्रथक-प्रथक अस्तित्व तो है और उनसे यत्किंचित् प्रतिफल भी प्राप्त होता है, पर वह रहता सर्वथा अपूर्ण एवं एकांगी ही है। बिजली के दोनों तार मिल कर ही प्रवाह पैदा करते हैं उसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सत्परिणाम उत्पन्न करता है। गायत्री उपासना में उत्कृष्ट जीवन के लिये अभीष्ट ज्ञान और कर्म का इस प्रकार समन्वय है कि उसे व्यक्तित्व के विकास का ऐसा समग्र शिक्षण कह सकते हैं जिसमें चिन्तन और कर्मकाण्ड का उपयुक्त सन्तुलन बहुत ही दूरदर्शिता के साथ मिलाकर रखा गया है।
उपासना काल में साधक का चिन्तन सर्वथा अन्तर्मुखी रहता है। बाहरी संसार का विचार और कर्म करते-करते ही पूरा समय बीतता है। पूजा पर्व का थोड़ा-सा समय इसके लिए सुरक्षित रखा गया है कि उस अवधि में मात्र अन्तर्मुखी चिन्तन किया जाय और अन्तर्जगत में सम्बन्धित तथ्यों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाय। जब तक इसी प्रयोजन में मन लगा रहता है तब तक साधना में मन लगा समझा जाता है। सन्तोष मिलता है और सत्परिणाम भी मिलता है किन्तु यदि मन थोड़े से समय में भी भौतिक जीवन का—वाह्य संसार का ही चिन्तन करने के लिये दौड़ता रहे तो समझना चाहिए साधना अधूरी रह गई। मनोनिग्रह की आवश्यकता इसी लिए समझी जाती है कि उस अवधि में जो कुछ सोचा और किया जाय वह आत्मिक क्षेत्र से ही सम्बन्धित हो। जितनी देर ऐसा बन पड़ता है समझा जाता है कि उपासना का उपक्रम ठीक तरह बन पड़ा। उपासना का पूर्वार्ध (1) स्वाध्याय (2) सत्संग (3) चिन्तन (4) मनन है। इनमें आत्म-समीक्षा, आत्म-सुधार, आत्म-निर्माण और आत्म-विकास के सन्दर्भ में विभिन्न समस्याओं का स्वरूप एवं समाधान समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसे साधना का तत्वज्ञान एवं दर्शन पक्ष कह सकते हैं। ब्रह्म-विद्या का सारा कलेवर इस प्रशिक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही खड़ा किया गया है। कथा, प्रवचनों का यही उद्देश्य है।
उपासना का उत्तरार्ध वह है जिसे कर्मकाण्ड उपचार के साथ सम्पन्न किया जाता है। इसके भी चार चरण हैं—(1) पवित्रीकरण (2) देव पूजन (3) जप (4) ध्यान। प्रायः इन्हीं चार वर्गों में ही साधना विधि-विधान आ जाता है। रुचि भिन्नता और परिस्थिति विशेष के कारण विभिन्न प्रकार के साधन विधान बनते रहे हैं। पर उन सबको यदि वर्गीकृत करना हो तो चार में उन सबका समावेश हो सकता है।
पवित्रीकरण में पवित्र नदी सरोवरों का स्नान, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, उपकरण शुद्धि आदि सम्मिलित हैं। पूजा उपचार आरम्भ करने से पहले आत्म शोधन के लिए मार्जन, आचमन, प्राणायाम, न्यास, अघमर्षण आदि की क्रियाएं सम्पन्न करनी पड़ती हैं। देव पूजन में प्रतिमा पूजन, षोडशोपचार, स्तवन, अभिषेक, आरती, परिक्रमा, मन्दिर दर्शन, सूर्यार्घदान, कलश स्थापना, दीप स्थापन, हवन आदि कृत्यों को गिना जा सकता है।
जप में मन्त्रों के रूप में जाने, जाने वाले शब्द गुच्छकों की रटन, पुनरावृत्ति, कीर्तन, मानसिक जप, सोहम् का अजपा जप, अखण्ड पारायण, ग्रन्थ पाठ आदि की गणना होती है।
ध्यान में बिन्दु योग, लययोग, नादयोग, चक्रवेधन, पंचकोश साधना, प्राणयोग, ऋणयोग, विन्दुयोग आदि वे सभी साधनाएं आ जाती हैं जिनमें चिन्तन को एक विशिष्ट दिशा धारा में प्रवाहित करना पड़ता है।
इस प्रकार समग्रयोग के आठ अंग हैं। भगवती साधना में दुर्गा की आठ भुजाओं के रूप में शास्त्रकारों ने इन्हीं का निरूपण किया है।
देखना यह है कि इन आठों क्रिया कृत्यों से किस प्रकार व्यक्तित्व का निखार और उभार सम्भव होता है। मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए इन विधि-विधानों का किस प्रकार—किस मर्मस्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्य दृष्टि से यह सभी उपचार जादुई लगते हैं और प्रतीत होता है कि इनमें कोई रहस्यमय प्रक्रिया भरी होगी, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। साधना विधियों को प्रतीक पूजा कहा गया है। इनके क्रिया कृत्यों में चिन्तन और कर्तृत्व में उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ने की भाव भरी प्रेरणाओं का समावेश है। इन प्रेरणाओं को जितना व्यावहारिक जीवन में उतारा जाता है, उसी अनुपात से अन्तर की दिव्य शक्तियां उभरती हैं और उस उभार के अनुरूप, सिद्धियां और विभूतियों के चमत्कारी प्रतिफल सामने आते हैं।
पवित्रीकरण के अन्तर्गत जल सिंचन, तीन आचमन, न्यास, अघमर्षण प्राणायाम आते हैं इनमें जल, वायु एवं अंग स्पर्श के माध्यम से अन्तरंग और बहिरंग की पवित्रता धारण करने के निर्देश हैं। शारीरिक कषाय और मानसिक कल्मष ही आत्मिक प्रगति के प्रमुख अवरोध हैं। उन्हें हटाने, समग्र स्वच्छता अपनाने से अन्तरात्मा में भगवान की अनुकम्पा एवं दिव्य समर्थता का अवतरण सम्भव होता है। यह तथ्य समझाने और अपनाने के लिए पवित्रीकरण के पांचों उपचार हैं।
दूसरा उपचार देव पूजन है। दूसरा तात्पर्य है देवत्व की गरिमा को स्वीकार करना और उसके सम्मुख नतमस्तक होना-पक्षधर बनना। आमतौर से सामान्य जीवन दैत्य उपासक ही रहता है। दैत्य अर्थात् वैभव, सुविधा साधन, लिप्सा-लालसा का तुष्टीकरण। इन्हीं कुचक्र में सारा श्रम और मनोयोग खप जाता है। देवत्व की कल्पना भर भले ही होती रहे, पर उसके परिपोषण के लिए कुछ बच ही नहीं पाता। इस पशु प्रवृत्ति को उलटने का संकल्प ही देव पूजन है। देवता की प्रतिमाओं के पीछे आदर्श भरे पड़े हैं। प्रतिमाएं एक प्रकार की पुस्तकें हैं जिनकी आकृतियों और प्रकृतियों के समुच्चय से यही बताया गया है कि देवानुयायी का चरित्र और चिन्तन कैसा होना चाहिए। देव पूजन में जो उपचार वस्तुएं काम आती हैं वे भी सद्गुणों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें अपनाने वाले पर देव कृपा बरसने का तथ्य प्रकट करती हैं। जल अर्थात् पवित्रता-तरलता। पुष्प अर्थात् कोमलता सुषमा। चन्दन अर्थात् उदारता, श्रद्धा। दीपक अर्थात् परमार्थ परायणता, प्रकाश प्रज्ञा। नैवेद्य अर्थात् मधुरता, अंशदान निष्ठा। अर्घ्यदान-श्रेष्ठता के प्रति समर्पण-विसर्जन। देवता के सम्मुख इन उपचारों को पूजा उपकरण के रूप में प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इन सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की अनिवार्य शर्त है जिसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्न किये ही जाने चाहिए।
जप का तात्पर्य है—अनवरत और अथक प्रयास एवं अभ्यास की निरन्तर पुनरावृत्ति। आमतौर से एक काम पर से मनुष्य का मन जल्दी ही ऊब जाता है और नवीनता की तलाश होने लगती है। चंचलता की यह वानर वृत्ति महान कार्यों के लिए आवश्यक अध्यवसाय बनने ही नहीं देती। उच्चस्तरीय कार्यों में बाल-क्रीड़ा जैसा कौतुक भी नहीं होता वे साधारण मनःस्थिति को नीरस ही लगते हैं। इसलिए क्षमता सम्पन्न व्यक्ति भी कोई महत्वपूर्ण कार्य—निरन्तर अध्यवसाय न अपना सकने के कारण कर नहीं पाते। आरम्भ भी करें तो मन की ऊब वैसा करने नहीं देती। इस मोर्चे को वही जीत सकता है जिसने मन जीता हो। कहते हैं कि जो अपने को जीतता है वही दूसरों को—संसार को—जीत पाता है। यहां मनोजप की ही चर्चा है। इसका अभ्यास जप के माध्यम से भली प्रकार हो सकता है। एक ही रटन को धैर्यपूर्वक देर तक करते रहने से नवीनता की तलाश के लिए उचक-मचक करने वाली वानर वृत्ति पर अंकुश लगता है और वह प्रवृत्ति जगती है जिसके अनुरूप नीरस दीखने वाले महान कार्यों पर धैर्यपूर्वक चित्त-वृत्तियों को जमाये रहा जा सके। यह चित्त-वृत्तियों का निरोध ही महर्षि पातंजलि के अनुसार योग है। योग साधना का प्रथम चरण जप माना गया है उससे शरीर और मन दोनों को धैर्यपूर्वक अनवरत क्रम से एक ही कार्य को करते रहने का स्वभाव बनता है। महत्वपूर्ण कार्य कर सकने के लिए यह अभ्यास नितान्त आवश्यक है।
जप के उपरान्त दूसरा चरण है ध्यान। शारीरिक गतिविधियों को जप के द्वारा अध्यवसाय रत रहने के लिए प्रशिक्षित अभ्यस्त किया जाता है। इसका अगला चरण है मन-मस्तिष्क। चिन्तन को एक केन्द्र पर नियोजित किये रहना—एक दिशाधारा में संलग्न रहना—यही है ध्यान धारणा का उद्देश्य। मन में कितनी प्रचण्ड शक्ति भरी पड़ी है किन्तु वह बिखराव से ही अस्त-व्यस्त और नष्ट-भ्रष्ट होती रहती हैं। यदि एकाग्रता पा सके तो सामान्य स्तर का मनुष्य भी विद्याध्ययन अनुभव सम्पादन—शोध कार्य—विशिष्ट कला-कौशलों का उपार्जन जैसी चमत्कारी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। एकाग्रता साधने वाले व्यक्ति ही वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, योग निष्णात होते देखे गये हैं। सांसारिक प्रयोजनों में भी महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने में एकाग्रता के अभ्यास की ही प्रधान भूमिका रहती है।
अन्तर्जगत की विभूतियां वाह्य जगत की सम्पदाओं से भी अधिक मूल्यवान हैं। समष्टिगत भौतिक सम्पदाएं जल, थल और आकाश में से निकालनी होती हैं। किन्तु व्यक्ति को विभूतिवान बना सकने के लिए जिन दिव्य उपलब्धियों की आवश्यकता होती है उन्हें अपने भीतर ही खोजा जा सकता है। दृष्टिकोण, मान्यताएं, आस्थाएं, इच्छाएं, आदतें, उमंगें, सम्वेदनाएं आदि की भाव सम्पदाएं ही मिलकर व्यक्तित्व को ढालती हैं और उसी आन्तरिक वैभव के आधार पर मनुष्य का वाह्य जीवन ढलता है। पिछड़ेपन और प्रगतिशीलता का उद्गम केन्द्र अन्तःक्षेत्र से ही प्रकट और प्रवाहित होता है। गढ़े खजाने की तरह मनुष्य जीवन की वास्तविक और बहुमूल्य सम्पदाएं उसके अन्तःक्षेत्र में ही भरी पड़ी हैं। इन्हें जानना, खोदना, उभारना और विकसित परिष्कृत करने का विज्ञान ही ध्यान योग है। ध्यान को अन्तर्जगत के अंधेरे में फेंकी जाने वाली सर्चलाइट कहा गया है। उस आधार पर उस दिव्य क्षेत्र की स्थिति को जानना और बिखरी पड़ी दिव्य सम्पदाओं को बटोर लाना सम्भव होता है।
आत्म-निरीक्षण, आत्म-सुधार, आत्म-निर्माण और आत्म-विकास का समुच्चय ही आत्मिक प्राप्ति है। उसी मार्ग पर चलते हुए अपूर्णता की पूर्णता में परिणिति और लक्ष्य प्राप्ति में सफलता सम्भव होती है। उस प्रसंग के सारे क्रिया-कलाप अन्तर्जगत में ही करने होते हैं और उनके लिए मानसिक एकाग्रता का प्रखर उपयोग ही कारगर सिद्ध होता है। ध्यान के द्वारा यही चेतनात्मक प्रखरता प्राप्त होती है और इसके द्वारा अन्तर्जगत में उपयोगी परिवर्तन परिष्कार कर सकना सम्भव होता है।
गायत्री उपासना का उत्तरार्ध आत्म-शोधन, देव-पूजन, जप और ध्यान है—इन चारों का उपयोग आत्म-निर्माण के लिए क्रिया योग के रूप में किया जाता है। उसे पूर्वार्ध का—स्वाध्याय सत्संग—मनन-चिन्तन का पूरक ही माना जाना चाहिए। व्यक्तित्व के समग्र विकास को ही भौतिक और आत्मिक सम्पदाओं का—ऋद्धि-सिद्धियों का केन्द्र माना गया है। उस प्रयोजन की पूर्ति में गायत्री उपासना का तत्वज्ञान और विधि-विधान असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है।
Write Your Comments Here:
- आत्मबल सम्पन्न व्यक्तित्व का निर्माण-गायत्री शक्ति से
- सूक्ष्म वातावरण के अनुकूलन की प्रचण्ड प्रक्रिया
- युग परिवर्तन के उपयुक्त वातावरण बनाना होगा
- युग परिवर्तन में गायत्री महाशक्ति का अवतरण
- युगशक्ति के रूप में गायत्री चेतना का अरुणोदय
- देवत्व का अवतरण युग साधना गायत्री के माध्यम से
- गायत्री उपासना से व्यक्तित्व का समग्र उत्कर्ष
- व्यक्तित्व के विकास में, गायत्री साधना का उपयोग
- गायत्री जप और उसकी सामूहिक शक्ति
- युग शक्ति का अवतरण और प्रसार विस्तार
- गायत्री ही गुरु मन्त्र है
- गायत्री अभियान से व्यक्ति और समाज का अभिनव निर्माण
- युग क्रान्ति में गायत्री यज्ञों की भूमिका
- त्रिपदा गायत्री—ब्रह्म विद्या की त्रिवेणी
- गायत्री की प्रथम प्रेरणा—श्रम व्यवस्था और संयम
- गायत्री की द्वितीय प्रेरणा-सद्विवेक, सत्साहस और स्वावलम्बन
- गायत्री की तृतीय प्रेरणा—एकता, समता, सहकारिता