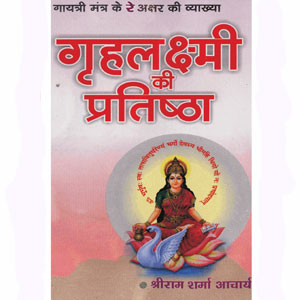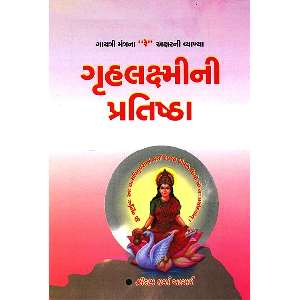गृहलक्ष्मी की प्रतिष्ठा 
विवाह आत्मविकास का प्रधान साधन है
Read Scan Versionहिंदू धर्म में जिन षोडश संस्कारों का विधान है, उनका ध्येय मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर उन्मुख करना है । वह जैसे-जैसे बड़ा होता है उसका आत्मभाव उभरता है और आत्मविस्तार प्रारंभ होता है । ज्यों-ज्यों वह आत्मदमन करता है, अपने ऊपर नियंत्रण लगाता है, त्याग करता है, त्यों-त्यों उसमें आत्मीयता का भाव बढ़ता जाता है । बड़ा होने पर उसका विवाह संस्कार होता है । यह होने पर मनुष्य के ऊपर अनेक जिम्मेदारियाँ आ पड़ती हैं । यहाँ तो देह भाव-विलोपन और आत्मबलिदान का पाठ पूरा-पूरा सीखना पड़ता है । कालांतर में जो संतान प्राप्त होती है, उसकी सेवा बिना आत्मत्याग और बलिदान के संभव नहीं । साथ-साथ अपने जीवन-सहचर के व्यक्तित्व में जो अपने व्यक्तित्व को मिलाना होता है-वह भी बिना आत्मोत्सर्ग के संभव नहीं । कदाचित अपने जीवन-सहचर के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को हमें विलीन भी करना पड़ता है - 'होमना भी पड़ता है और यह देहभाव को बनाए रखकर नहीं बन सकता । इस जीवन में तो इच्छा निरोध, आत्म- संयम की पूरी-पूरी साधना करनी पड़ती है क्योंकि बिना इसके अपने जीवन-सहचर के साथ पूर्णतया घुल-मिल जाना नहीं बनता । अतएव विवाह में आत्म-विलीनीकरण परमावश्यक है और यह आत्म-विलीनीकरण देहभाव का यह उच्छेद-पशुत्व को दबाने और देवत्व को जगाने का एक साधन है । अतएव विवाह पशुत्व से देवत्व की ओर बढ़ने का एक मार्ग है ।
विवाह भौतिक दृष्टि के अतिरिक्त, आध्यात्मिक जीवन के क्रमिक विकास की दृष्टि से भी जीव के बाल्यकाल के पश्चात स्वाभाविक रूप से ही आवश्यक है । बाल्यकाल के उपरांत आध्यात्मिक सोपान पर आगे चढ़ने के लिए जो अगली सीढ़ी हो सकती है- वह विवाह-बंधन ही है । बाल्यकाल के उपरांत एकदम संन्यास धर्म में पहुँचना सबके लिए सरल नहीं और न अपेक्षित ही है । बाल्यकाल में सदा खाते-पीते, सोते-जागते सुखों का उपभोग ही होता-इंद्रियों की तृप्ति का प्रयत्न ही चलता रहता है । इच्छाओं का निरोध नहीं होता, किंतु इसके ठीक विपरीत संन्यास में एकदम त्याग ही त्याग है । अतएव विवाह ही एक ऐसी बीच की अवस्था है, जो मनुष्य को विरक्ति और भोग की अवस्था के ठीक बीचोबीच रखकर विरक्ति और त्याग के साथ-साथ ही सुख-भोग की शिक्षा देती है । मध्यम मार्ग इस जीवन में ही संभव है । राग-द्वेष से विमुक्त होकर सुखोपभोग करना इस जीवन के अतिरिक्त न तो बाल्यावस्था में संभव है और न संन्यासावस्था में । इसलिए विवाह एक पवित्र बंधन है और विवाहित जीवन को योग्यतापूर्वक निभाने में ही मनुष्य का आध्यात्मिक कल्याण है ।
सफल विवाहित जीवन ईश्वर से सम्मिलिन की पूर्वावस्था है । जायसी आदि संतों ने ईश्वर-प्रेम कैसा होना चाहिए उसकी एक क्षुद्र झाँकी पति-पत्नी के प्रेम को माना है । जब लौकिक प्रेम के निभाने में इतने बलिदान की आवश्यकता होती है तो ईश्वर-प्रेम तो फिर सिर का सौदा है, सिर हथेली पर रखकर चलना है । अतएव लौकिक प्रेम ही ईश्वर से सामीप्य लाभ करने का मार्ग प्रशस्त करता है । तैत्तिरीयोपनिषद् में तो 'प्रजातंतु मा व्यवच्छेत्सीः' ऐसा उपदेश है । अतएव जहाँ पवित्र जीवन है, वहाँ पापमय उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है ? फिर हम ब्रह्मज्ञान हो जाने पर भी सत्काम जाबाल और समुग्वारैक्य जैसे ब्रह्मज्ञानियों को भी विवाह करते देखते हैं । इससे भी विवाहित जीवन की पवित्रता ही प्रतिपादित होती है । केवल आत्मसंयम का होना न होना ही विवाहित जीवन को पवित्र या अपवित्र बना देता है । पुनश्च भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है "धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ" अर्थात प्राणियों में स्थित अविरुद्ध काम हूँ ।
ऋग्वेद का वचन है-
समानी व आकूति: समाना हृदयानि व: । समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसाहसति । ।
अर्थात हमारा आचरण समान हो, हमारे हृदय समान हों, हमारे मन समान हों और हम एकदूसरे की सहायता के लिए सदा तत्पर रहें । यदि हम अपने जीवन-सहचर के साथ भी एकात्मता और अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकते तो वेद में वर्णित समाज के साथ इतनी अभिन्नता हो सकना तो बहुत दूर की बात है । इस दृष्टि से भी विचार करें तो विवाह-बंधन उत्कृष्ट सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवनयापन करने के लिए उत्तम शिक्षण-स्थल है । विवाह आध्यात्मिक विकास के लिए सुअवसर प्रदान करता है ।
विवाह जीवन बहुतों के लिए दुःखमय प्रतीत होता है । किंतु इसका कारण केवल आत्मसंयम और पुरुषार्थ की कमी है । कठिनाइयाँ केवल हमारी चरितगत तथा पुरुषार्थ संबंधी न्यूनताओं की ओर ही संकेत करती हैं और मानो हमें उन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्बोधित करती हैं । जो लोग पलायन-मनोवृत्ति लेकर विवाह-बंधन से बच निकलते हैं, वे दुःख और कठिनाइयों से भी भले ही बच निकलें, किंतु कठिनाइयों से बच निकलना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है । इससे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती । जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मशक्ति बढ़ाना और अपनी उन चरित्रगत तथा पुरुषार्थ संबंधी न्यूनताओं को दूर करना, जो कठिनाइयों का जन्म देती हैं और जिनके रहते हुए कठिनाइयाँ प्रतीत होती हैं । विवाहित जीवन की उपेक्षा कर तथा अपनी चरित्रगत न्यूनताओं के ज्ञान से अपरिचित रहकर पूर्ण आनंद भोगने का दावा करना भ्रममात्र है । पूर्ण आनंद तो पूर्णतया पुरुषार्थी और दोषमुक्त होने पर ही प्राप्त हो सकता है । विवाह पुरुषार्थी और पूर्णतया दोषमुक्त होने का बढ़िया साधन है । अतएव जिनके जीवन में कोई दोष नहीं और जो पूर्ण पुरुषार्थी हैं केवल वे ही इस बीच की सीढ़ी-विवाहित जीवन की उपेक्षा करने के लिए के अधिकारी हैं, क्योंकि उनको विवाहित जीवन फल आत्मविजय पहले प्राप्त ही रहता है ।
मनुष्य ने अपने विकास काल में जिस सर्वोत्तम तत्व को विकसित किया है, वह माता-पिता का हृदय ही है । इसमें जिस सुकोमलता का निवास है, वह मनुष्य को देवोपम बना सकती है । इसी के कारण मनुष्य इस हिंसक विश्व में सर्वोपरि सुशोभित हो रहा है । इस प्रेममय हृदय की प्राप्ति के लिए विवाह ही द्वार को उन्मुक्त करता है ।
Write Your Comments Here:
- गृहलक्ष्मी की प्रतिष्ठा
- नारी के सहयोग के बिना भर अपूर्ण रहता है
- विवाह की उपयोगिता
- विवाह आत्मविकास का प्रधान साधन है
- हमारा वैवाहिक जीवन कैसे सुखी हो सकता है ?
- वैवाहिक जीवन का उत्तरदायित्व
- उत्तरदायित्व का निर्वाह
- दो स्वर्णिम सूत्र
- गृहस्थ जीवन की सफलता
- दांपत्य जीवन में कलह से बचिए
- विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन
- पत्नी का सदैव सम्मान कीजिए
- स्त्रियोचित शिक्षा की आवश्यकता