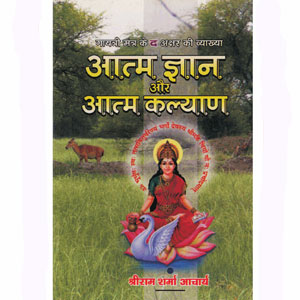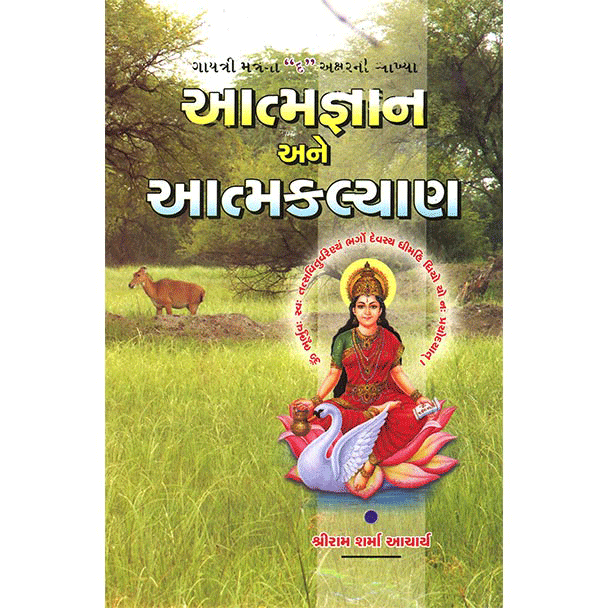आत्मज्ञान और आत्म कल्याण 
आत्मकल्याण के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता
Read Scan Version
आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने वाले को आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति अत्यावश्यक है । इसका आशय यह है कि हमको विवेक के प्रकाश में अपने दोषों पर विचार करना और उनको दूर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए । इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण बिना निर्दोषता की प्राप्ति हो सकना बहुत कठिन है ।
अपना निरीक्षण करने पर असत्य का ज्ञान एवं सत्य से एकता और प्राप्त बल तथा योग्यता का सदुपयोग स्वतः होने लगता है । यदि हम असत्य को नहीं देख पाएँ अथवा सत्य से अभिन्न एवं अपने कर्त्तव्य से परिचित नहीं हुए तो समझना चाहिए कि हमने अपना निरीक्षण नहीं किया । अपना यथेष्ट निरीक्षण करने पर किसी अन्य गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं रहती, कारण कि जिसके प्रकाश में सबका सब कुछ हो रहा है, उसमें अनंत शक्ति विद्यमान है । अपना निरीक्षण करते-करते प्राणी उससे अभिन्न हो जाता है, जो वास्तव में सबका सब कुछ होते हुए भी सबसे अतीत है । अपना निरीक्षण हमें बल के सदुपयोग और विवेक के आदर की प्रेरणा देता है । बल के सदुपयोग से निर्बलताएँ और विवेक के आदर से अविवेक स्वत: मिट जाता है ।
प्रत्येक प्राणी अपने से अधिक बलवानों के किसी भी प्रकार के बल की अपने प्रति सदुपयोग की आशा करता है, किंतु वह स्वयं अपने प्राप्त बल का निर्बलों के प्रति दुरुपयोग करता है तो वह स्वयं अपने प्राप्त विवेक का अनादर नहीं तो और क्या है ?
बल का अर्थ है सभी प्रकार के अर्थात- तनबल, धनबल, विद्याबल और पद अथवा प्रभुता बल इत्यादि । धन के दुरुपयोग से ही समाज में निर्धनता, शिक्षा अर्थात ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के दुरुपयोग से समाज में अविवेक की वृद्धि तनबल के दुरुपयोग से समाज में हिंसा और चोरी, प्रभुता के दुरुपयोग से विरोधी शासन का जन्म आदि दुर्गुणों की वृद्धि होती है ।
प्रत्येक प्राणी को अपनी रक्षा स्वभावत: प्रिय है, फिर भी वह स्वयं अहिंसक न रहकर हिंसा में प्रवृत्त होता है, जिससे हृदय बैर भाव से भर जाता है, जो संघर्ष का मूल है । अत: संघर्ष मिटाने के लिए प्रत्येक भाई-बहनों को अपना हृदय बैर भाव से रहित करना होगा । बैर भाव से रहित होने के लिए अहिंसक होना अत्यंत आवश्यक है । अपनी रक्षा की प्रियता का विवेक हमें अहिंसक होने की प्रेरणा देता है, जो अनादि सत्य है । पर आज तो हम वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा हिंसात्मक प्रयोगों से संघर्ष मिटाने की बात सोच रहे हैं, जो सर्वथा असंभव है, कारण कि विवेक के अनादर से ही प्राणी के मन से संघर्ष उत्पन्न होता है । अतएव जब तक विवेकपूर्वक मन का संघर्ष न मिटेगा, तब तक समाज में होने वाले संघर्ष कभी नहीं मिट सकते चाहे वे वैज्ञानिक हों या कौटुंबिक अथवा सामाजिक ।
प्रत्येक अपराधी अपने प्रति क्षमा की आशा करता है और दूसरों को दंड देने की व्यवस्था चाहता है । यह अपने प्रति जो दूसरों से अहिंसक निर्भय, उदार क्षमाशील, त्यागी, सत्यवादी और विनम्रता आदि दिव्य गुणों से पूर्ण व्यवहार की आशा करता है, किंतु स्वयं उसी प्रकार का सद्व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं कर पाता । अपने प्रति मधुरता युक्त सम्मान की आशा करता है, पर दूसरों के प्रति अपमान एवं कटुतापूर्ण असद्व्यवहार करता है, तो वास्तव में भूल है । इसका परिणाम यह होता है कि प्राणी अपने प्रति रागी और दूसरों के प्रति दोषी हो जाता है जो सभी दुःखों का मूल है ।
अपने प्रति होने वाले अन्याय को सहन करते हुए यदि अन्यायकर्त्ता को क्षमा कर दिया जाय तो द्वेष, प्रेम में बदल जाता है । अपने द्वारा होने वाले अन्याय से स्वयं पीडि़त होकर जब उससे, जिसके प्रति अन्याय हो गया है क्षमा माँग ली जाय और इस प्रकार उससे क्षमा माँगते हुए अपने प्रति न्याय कर स्वयं दंड स्वीकार कर लिया जाय तो राग, त्याग में बदल जाता है ।
जब राग और द्वेष त्याग और प्रेम में बदल जाते हैं, तब मुक्ति की प्राप्ति स्वत: ही हो जाती है अथवा यों कहो कि अभिन्नता और असंगतता स्वत: आ जाती है । यही वास्तविक आनंद है ।
अपना निरीक्षण करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब हम राग से प्रेरित होकर इंद्रियों की ओर गतिशील होते हैं, तब इंद्रियजन्य ज्ञान के आधार पर हमें अनेक प्रकार की विषमताओं का भास होता है और इंद्रियजन्य स्वभाव में प्रवृत्त होने से हम क्रियाजन्य सुख की आसक्ति तथा परतंत्रता, जड़ता आदि में भी आबद्ध हो जाते हैं । इतना ही नहीं, अंत में हम शक्तिहीनता का अनुभव कर स्वाभाविक विश्राम अर्थात निवृत्ति को अपनाते हैं जिसके फलस्वरूप शक्तिहीनता मिटती जाती है और बिना प्रयत्न के आवश्यक शक्ति की उपलब्धि हो जाती है । यदि शक्तिहीनता, जड़ता विषमता इत्यादि दुःखों से दुखी होकर हम निवृत्ति द्वारा संचित शक्ति का व्यय न करके विषयों से विमुख होकर अंतर्मुख हो जावें तो भोग-योग में, जड़ता-चेतना में, विषमता-समता में, पराधीनता- स्वाधीनता में और अनेकता-एकता में बदल जाती है । फिर स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति एवं अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति स्वत: ही हो जाती है जो मानव की माँग है ।
अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति का यथेष्ट स्पष्ट परिचय प्राप्त करना ही वास्तविक आत्मनिरीक्षण है । उसके बिना हम अपने को निर्दोष बना ही नहीं सकते । मानव में दोष-दर्शन की दृष्टि स्वत: विद्यमान है, पर प्रमादवश प्राणी उसका उपयोग अपने जीवन पर न करके अन्य पर करने लगता है, जिसका परिणाम बडा ही भयंकर एवं दुःखद सिद्ध होता है । पराये दोष देखने से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि प्राणी अपने दोष देखने से वंचित हो जाता है और मिथ्याभिमान में आबद्ध होकर हृदय में घृणा उत्पन्न कर लेता है । यद्यपि हृदय प्रीति का स्थल है, घुणा का नहीं, पर ऐसा तभी संभव है जब मानव पराये दोष न देखकर अपने दोष देखने में सतत प्रयत्नशील रहे । अपने तथा पराये दोष देखने में एक बडा अंतर यह है कि पराये दोष देखते समय हम दोषों से संबंध जोड़ लेते हैं । जिससे कालांतर में स्वयं दोषी बन जाते हैं, पर अपना दोष देखते ही हम अपने को दोषों से असंग कर लेते हैं, जिससे स्वत: निर्दोषता आ जाती है, जो सभी को प्रिय है । अत: यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि दोष दर्शन की दृष्टि का उपयोग केवल अपने ही जीवन पर करना है, किसी अन्य पर नहीं ।
यद्यपि अनादि सत्य बीज रूप से प्रत्येक मानव में विद्यमान है, पर उसका आदर न करने से प्राणी उस सत्य से विमुख हो गया है और परिवर्तनशील वस्तु अवस्था एवं परिस्थितियों में आबद्ध होकर उनने अपने को दीन-हीन तथा अभिमानी और परतंत्र बना लिया है । इस दुखद बंधन से छुटकारा पाने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि प्राणी प्राप्त विवेक के प्रकाश में (जो चिर सत्य है) अपनी दशा का निरीक्षण करे और वस्तु अवस्था आदि से असंग होकर दुराचार को सदाचार में परिवर्तित करके अपने को निर्विकार बनाए ।
यह प्रत्येक मानव का अनुभव है कि दृश्य का संबंध सुख-दु:ख में आबद्ध करता है और दृश्य से असंग होने पर किसी प्रकार का दुःख शेष नहीं रहता है । प्रिय-से-प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति से संबंध स्वीकार करने पर भी प्राणी अपने को अलग करना चाहता है, कारण कि सबसे अलग हुए बिना वह चिर शांति तथा शक्ति नहीं प्राप्त कर पाता जो उसे स्व भाव से ही प्रिय है । यह निर्विवाद सिद्ध है ? कि प्राणी प्रिय-से-प्रिय प्रवृत्ति से थककर गहरी नींद के लिए प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु आदि से अलग होना चाहता है । यद्यपि सुषुप्ति में किसी भी प्रकार का वैषम्य तथा दु:ख शेष नहीं रहता, तथापि उससे भी प्राणी स्वयं उपराम हो जाता है और किसी ऐसी अवस्था की खोज करता है, जिसमें सुषुप्ति के समान साम्य तथा दु:खरहितता तो हो, किंतु संज्ञाशून्यता न हो । उस स्थिति के उपलब्ध हो जाने पर जब वह उससे भी उत्थान देखता है, तब उत्थान रहित, अलौकिक अनंत, नित्य, चिन्मय जीवन के लिए व्याकुल होता है अर्थात निर्विकल्प स्थिति से निर्विकल्प बोध की लालसा करता है, जो सभी अवस्थाओं से अतीत और स्वत सिद्ध है । इस स्वत: सिद्ध अनंत जीवन की रुचि मानव मात्र में स्वभाव से विद्यमान है । इसके लिए सभी अवस्थाओं से विमुख होना अनिवार्य है । अवस्थाओं से विमुख होते ही, इस अवस्थातीत जीवन का अनुभव हो जाता है ।
अपना निरीक्षण ही वास्तविक सत्संग, स्वाध्याय और अध्ययन है, कारण कि अपने निरीक्षण के बिना प्राणी किसी ऐसे सत्य, तत्व एवं ज्ञान की उपलब्धि ही नहीं कर सकता जो उसमें स्वयं न हो । अत: अपने निरीक्षण द्वारा ही हम वास्तविक सत्य तथा तत्व -एवं ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं ।
अपना निरीक्षण करते ही जिस विवेक से असत्य का दर्शन होता है, वही विवेक उसे सत्य से अभिन्न भी कर सकता है और उसी के द्वारा सत्य से अभिन्न और असत्य से निवृत्त होने का उपाय प्राप्त होता है । आत्मनिरीक्षण के बिना कोई भी सद्ग्रंथ तथा सद्गुरु से मिला प्रकाश अपने काम नहीं आता । वह केवल मस्तिष्क का संग्रह बन जाता है जो कि नक्शे की नदी के तुल्य है प्रत्येक नक्शा हमें वास्तविकता तक पहुँचने का साधन अवश्य है परंतु उसे देखकर संतोष करने से न तो एक बूँद जल मिलेगा न प्यास बुझेगी ।
अपने निरीक्षण के साथ-साथ ही हमें सद्ग्रंथ तथा सत्पुरुषों के प्रकाश का उपयोग करना चाहिए । आत्मनिरीक्षण द्वारा जब हम अपनी सभी प्रियताओं को जान लेते हैं, तब फिर हमारे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा नहीं होती, जिसमें दूसरे की प्रियता तथा हित निहित हो ।
अपना निरीक्षण करने पर हमें यह भलीभांति विदित हो जाता है कि प्राप्त शक्ति का सद्व्यय प्राणियों को स्वभाव से ही प्रिय है, कारण कि जब कोई हमारे साथ व्यवहार करता है, यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो तो तब हम उसके उस व्यवहार को उचित नहीं मानते, यद्यपि वही व्यवहार प्रमादवश हम स्वयं दूसरों के प्रति कर बैठते हैं ।
अपना निरीक्षण करने पर असत्य का ज्ञान एवं सत्य से एकता और प्राप्त बल तथा योग्यता का सदुपयोग स्वतः होने लगता है । यदि हम असत्य को नहीं देख पाएँ अथवा सत्य से अभिन्न एवं अपने कर्त्तव्य से परिचित नहीं हुए तो समझना चाहिए कि हमने अपना निरीक्षण नहीं किया । अपना यथेष्ट निरीक्षण करने पर किसी अन्य गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं रहती, कारण कि जिसके प्रकाश में सबका सब कुछ हो रहा है, उसमें अनंत शक्ति विद्यमान है । अपना निरीक्षण करते-करते प्राणी उससे अभिन्न हो जाता है, जो वास्तव में सबका सब कुछ होते हुए भी सबसे अतीत है । अपना निरीक्षण हमें बल के सदुपयोग और विवेक के आदर की प्रेरणा देता है । बल के सदुपयोग से निर्बलताएँ और विवेक के आदर से अविवेक स्वत: मिट जाता है ।
प्रत्येक प्राणी अपने से अधिक बलवानों के किसी भी प्रकार के बल की अपने प्रति सदुपयोग की आशा करता है, किंतु वह स्वयं अपने प्राप्त बल का निर्बलों के प्रति दुरुपयोग करता है तो वह स्वयं अपने प्राप्त विवेक का अनादर नहीं तो और क्या है ?
बल का अर्थ है सभी प्रकार के अर्थात- तनबल, धनबल, विद्याबल और पद अथवा प्रभुता बल इत्यादि । धन के दुरुपयोग से ही समाज में निर्धनता, शिक्षा अर्थात ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के दुरुपयोग से समाज में अविवेक की वृद्धि तनबल के दुरुपयोग से समाज में हिंसा और चोरी, प्रभुता के दुरुपयोग से विरोधी शासन का जन्म आदि दुर्गुणों की वृद्धि होती है ।
प्रत्येक प्राणी को अपनी रक्षा स्वभावत: प्रिय है, फिर भी वह स्वयं अहिंसक न रहकर हिंसा में प्रवृत्त होता है, जिससे हृदय बैर भाव से भर जाता है, जो संघर्ष का मूल है । अत: संघर्ष मिटाने के लिए प्रत्येक भाई-बहनों को अपना हृदय बैर भाव से रहित करना होगा । बैर भाव से रहित होने के लिए अहिंसक होना अत्यंत आवश्यक है । अपनी रक्षा की प्रियता का विवेक हमें अहिंसक होने की प्रेरणा देता है, जो अनादि सत्य है । पर आज तो हम वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा हिंसात्मक प्रयोगों से संघर्ष मिटाने की बात सोच रहे हैं, जो सर्वथा असंभव है, कारण कि विवेक के अनादर से ही प्राणी के मन से संघर्ष उत्पन्न होता है । अतएव जब तक विवेकपूर्वक मन का संघर्ष न मिटेगा, तब तक समाज में होने वाले संघर्ष कभी नहीं मिट सकते चाहे वे वैज्ञानिक हों या कौटुंबिक अथवा सामाजिक ।
प्रत्येक अपराधी अपने प्रति क्षमा की आशा करता है और दूसरों को दंड देने की व्यवस्था चाहता है । यह अपने प्रति जो दूसरों से अहिंसक निर्भय, उदार क्षमाशील, त्यागी, सत्यवादी और विनम्रता आदि दिव्य गुणों से पूर्ण व्यवहार की आशा करता है, किंतु स्वयं उसी प्रकार का सद्व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं कर पाता । अपने प्रति मधुरता युक्त सम्मान की आशा करता है, पर दूसरों के प्रति अपमान एवं कटुतापूर्ण असद्व्यवहार करता है, तो वास्तव में भूल है । इसका परिणाम यह होता है कि प्राणी अपने प्रति रागी और दूसरों के प्रति दोषी हो जाता है जो सभी दुःखों का मूल है ।
अपने प्रति होने वाले अन्याय को सहन करते हुए यदि अन्यायकर्त्ता को क्षमा कर दिया जाय तो द्वेष, प्रेम में बदल जाता है । अपने द्वारा होने वाले अन्याय से स्वयं पीडि़त होकर जब उससे, जिसके प्रति अन्याय हो गया है क्षमा माँग ली जाय और इस प्रकार उससे क्षमा माँगते हुए अपने प्रति न्याय कर स्वयं दंड स्वीकार कर लिया जाय तो राग, त्याग में बदल जाता है ।
जब राग और द्वेष त्याग और प्रेम में बदल जाते हैं, तब मुक्ति की प्राप्ति स्वत: ही हो जाती है अथवा यों कहो कि अभिन्नता और असंगतता स्वत: आ जाती है । यही वास्तविक आनंद है ।
अपना निरीक्षण करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब हम राग से प्रेरित होकर इंद्रियों की ओर गतिशील होते हैं, तब इंद्रियजन्य ज्ञान के आधार पर हमें अनेक प्रकार की विषमताओं का भास होता है और इंद्रियजन्य स्वभाव में प्रवृत्त होने से हम क्रियाजन्य सुख की आसक्ति तथा परतंत्रता, जड़ता आदि में भी आबद्ध हो जाते हैं । इतना ही नहीं, अंत में हम शक्तिहीनता का अनुभव कर स्वाभाविक विश्राम अर्थात निवृत्ति को अपनाते हैं जिसके फलस्वरूप शक्तिहीनता मिटती जाती है और बिना प्रयत्न के आवश्यक शक्ति की उपलब्धि हो जाती है । यदि शक्तिहीनता, जड़ता विषमता इत्यादि दुःखों से दुखी होकर हम निवृत्ति द्वारा संचित शक्ति का व्यय न करके विषयों से विमुख होकर अंतर्मुख हो जावें तो भोग-योग में, जड़ता-चेतना में, विषमता-समता में, पराधीनता- स्वाधीनता में और अनेकता-एकता में बदल जाती है । फिर स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति एवं अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति स्वत: ही हो जाती है जो मानव की माँग है ।
अपनी वर्तमान वस्तुस्थिति का यथेष्ट स्पष्ट परिचय प्राप्त करना ही वास्तविक आत्मनिरीक्षण है । उसके बिना हम अपने को निर्दोष बना ही नहीं सकते । मानव में दोष-दर्शन की दृष्टि स्वत: विद्यमान है, पर प्रमादवश प्राणी उसका उपयोग अपने जीवन पर न करके अन्य पर करने लगता है, जिसका परिणाम बडा ही भयंकर एवं दुःखद सिद्ध होता है । पराये दोष देखने से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि प्राणी अपने दोष देखने से वंचित हो जाता है और मिथ्याभिमान में आबद्ध होकर हृदय में घृणा उत्पन्न कर लेता है । यद्यपि हृदय प्रीति का स्थल है, घुणा का नहीं, पर ऐसा तभी संभव है जब मानव पराये दोष न देखकर अपने दोष देखने में सतत प्रयत्नशील रहे । अपने तथा पराये दोष देखने में एक बडा अंतर यह है कि पराये दोष देखते समय हम दोषों से संबंध जोड़ लेते हैं । जिससे कालांतर में स्वयं दोषी बन जाते हैं, पर अपना दोष देखते ही हम अपने को दोषों से असंग कर लेते हैं, जिससे स्वत: निर्दोषता आ जाती है, जो सभी को प्रिय है । अत: यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि दोष दर्शन की दृष्टि का उपयोग केवल अपने ही जीवन पर करना है, किसी अन्य पर नहीं ।
यद्यपि अनादि सत्य बीज रूप से प्रत्येक मानव में विद्यमान है, पर उसका आदर न करने से प्राणी उस सत्य से विमुख हो गया है और परिवर्तनशील वस्तु अवस्था एवं परिस्थितियों में आबद्ध होकर उनने अपने को दीन-हीन तथा अभिमानी और परतंत्र बना लिया है । इस दुखद बंधन से छुटकारा पाने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि प्राणी प्राप्त विवेक के प्रकाश में (जो चिर सत्य है) अपनी दशा का निरीक्षण करे और वस्तु अवस्था आदि से असंग होकर दुराचार को सदाचार में परिवर्तित करके अपने को निर्विकार बनाए ।
यह प्रत्येक मानव का अनुभव है कि दृश्य का संबंध सुख-दु:ख में आबद्ध करता है और दृश्य से असंग होने पर किसी प्रकार का दुःख शेष नहीं रहता है । प्रिय-से-प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति से संबंध स्वीकार करने पर भी प्राणी अपने को अलग करना चाहता है, कारण कि सबसे अलग हुए बिना वह चिर शांति तथा शक्ति नहीं प्राप्त कर पाता जो उसे स्व भाव से ही प्रिय है । यह निर्विवाद सिद्ध है ? कि प्राणी प्रिय-से-प्रिय प्रवृत्ति से थककर गहरी नींद के लिए प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु आदि से अलग होना चाहता है । यद्यपि सुषुप्ति में किसी भी प्रकार का वैषम्य तथा दु:ख शेष नहीं रहता, तथापि उससे भी प्राणी स्वयं उपराम हो जाता है और किसी ऐसी अवस्था की खोज करता है, जिसमें सुषुप्ति के समान साम्य तथा दु:खरहितता तो हो, किंतु संज्ञाशून्यता न हो । उस स्थिति के उपलब्ध हो जाने पर जब वह उससे भी उत्थान देखता है, तब उत्थान रहित, अलौकिक अनंत, नित्य, चिन्मय जीवन के लिए व्याकुल होता है अर्थात निर्विकल्प स्थिति से निर्विकल्प बोध की लालसा करता है, जो सभी अवस्थाओं से अतीत और स्वत सिद्ध है । इस स्वत: सिद्ध अनंत जीवन की रुचि मानव मात्र में स्वभाव से विद्यमान है । इसके लिए सभी अवस्थाओं से विमुख होना अनिवार्य है । अवस्थाओं से विमुख होते ही, इस अवस्थातीत जीवन का अनुभव हो जाता है ।
अपना निरीक्षण ही वास्तविक सत्संग, स्वाध्याय और अध्ययन है, कारण कि अपने निरीक्षण के बिना प्राणी किसी ऐसे सत्य, तत्व एवं ज्ञान की उपलब्धि ही नहीं कर सकता जो उसमें स्वयं न हो । अत: अपने निरीक्षण द्वारा ही हम वास्तविक सत्य तथा तत्व -एवं ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं ।
अपना निरीक्षण करते ही जिस विवेक से असत्य का दर्शन होता है, वही विवेक उसे सत्य से अभिन्न भी कर सकता है और उसी के द्वारा सत्य से अभिन्न और असत्य से निवृत्त होने का उपाय प्राप्त होता है । आत्मनिरीक्षण के बिना कोई भी सद्ग्रंथ तथा सद्गुरु से मिला प्रकाश अपने काम नहीं आता । वह केवल मस्तिष्क का संग्रह बन जाता है जो कि नक्शे की नदी के तुल्य है प्रत्येक नक्शा हमें वास्तविकता तक पहुँचने का साधन अवश्य है परंतु उसे देखकर संतोष करने से न तो एक बूँद जल मिलेगा न प्यास बुझेगी ।
अपने निरीक्षण के साथ-साथ ही हमें सद्ग्रंथ तथा सत्पुरुषों के प्रकाश का उपयोग करना चाहिए । आत्मनिरीक्षण द्वारा जब हम अपनी सभी प्रियताओं को जान लेते हैं, तब फिर हमारे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा नहीं होती, जिसमें दूसरे की प्रियता तथा हित निहित हो ।
अपना निरीक्षण करने पर हमें यह भलीभांति विदित हो जाता है कि प्राप्त शक्ति का सद्व्यय प्राणियों को स्वभाव से ही प्रिय है, कारण कि जब कोई हमारे साथ व्यवहार करता है, यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो तो तब हम उसके उस व्यवहार को उचित नहीं मानते, यद्यपि वही व्यवहार प्रमादवश हम स्वयं दूसरों के प्रति कर बैठते हैं ।