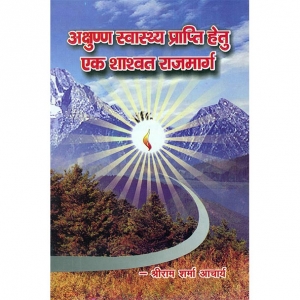अक्षुण्ण स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु एक शाश्वत राजमार्ग 
सात्विकता को भुला न दिया जाय
मानवी सत्ता जिस प्रकार सम्वेदनशील है, उसी प्रकार उसके आहार में भी सम्पर्क क्षेत्र का प्रभाव ग्रहण करने की क्षमता है। इसी बात को यों भी कह सकते हैं कि मनुष्य का पाचन तन्त्र विलक्षण है, वह न केवल आहार से शारीरिक पोषण करता है, वरन् उसमें सन्निहित सूक्ष्म शक्ति एवं सम्वेदना भी ग्रहण करता है। जब कि अन्य प्राणी शरीर प्रधान होने के कारण मात्र रक्त-मांस ही प्राप्त करते हैं।
यों चेतना के सम्पर्क से प्रभावित तो सभी पदार्थ होते हैं, पर यह विशेषता मानवी आहार में विशेष रूप से पाई जाती है, वह उगाने, पकाने, परोसने वाले व्यक्तियों से प्रभावित होती है। स्थानों में संव्याप्त भिन्न-भिन्न प्रकार के वातावरण उस पर अपनी छाप छोड़ते हैं। फलतः वह जिसके पेट में जाता है, उसके न केवल शरीर में वरन् मनः संस्थान में भी भली-बुरी विशेषतायें उत्पन्न करता है, जो अपने भीतर अर्जित कर रखी थीं।
एक पुरानी लोकोक्ति है—जैसा खाये अन्न वैसा बने मन। तात्पर्य यह है कि आहार के साथ जुड़ी हुई विशेषतायें न केवल शरीर को वरन् मन को भी प्रभावित करती हैं। चिन्तन के प्रवाह में हेर-फेर करती हैं। दृष्टिकोण को, स्वभाव को, रुझान को, मोड़ने-मरोड़ने में अपने स्तर का समावेश करती हैं। आहार में पाये जाने वाले पोषक पदार्थों की तालिका से परिचित यह जानते हैं कि इसका खाने वाले के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहलवानों के लिए चिकनाई अधिक उपयोगी पड़ती है और मरीज के लिए सुपाच्य दाल दलिया-शाकाहार-फलाहार। बालकों को एक स्तर का आहार दिया जाता है, तो प्रौढ़ों को दूसरी तरह का, वृद्धों को तीसरी तरह का। यह निर्धारण शरीरों की स्थिति एवं आवश्यकता का ताल-मेल बिठाते हुए किया जाता है। पशुओं को कड़ी मेहनत की थकान उतारने के लिए एक तरह का चारा-दाना दिया जाता है, तो दूध उतरने के लिए दूसरी तरह का। बकरी और हाथी के लिए भी उनके अनुरूप खाद्य जुटाना पड़ता है। उसमें भिन्नता इस आधार पर रहती है कि उसकी पाचन प्रकृति कैसी है और पेट कितनी मात्रा में भरता है। यही बात मनुष्य के संबंध में भी है, उनकी शारीरिक मांग और पाचन की स्थिति देखते हुए निर्णय करना पड़ता है कि कौन क्या खाये कितना खाये?
यहां विचारणीय विषय है कि मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तन्त्र मन संस्थान को प्रभावित करने में आहार की क्या विशेष भूमिका होती है। इस सम्बन्ध में कुछ गहराई में उतरने की आवश्यकता है। मोटी बुद्धि तो इतना ही सोच सकती है कि शरीर के अन्यान्य अवयवों की भांति मस्तिष्क भी एक अंग है जिस रस-रक्त से समूचे शरीर को पोषण मिलता है, उसी स्तर का, उसी अनुपात का प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ना चाहिए। इस जानकारी में कोई विवाद जैसी बात नहीं है, तो भी दृष्टव्य यह है कि क्या चिन्तन क्षेत्र की कल्पना, बुद्धिमता, दूरदर्शिता, नीतिमत्ता, मान्यता, आकांक्षा एवं प्रकृति जैसी विशेषताओं को भी आहार का स्तर कुछ प्रभावित करता है क्या? स्तर से तात्पर्य है मानवी गरिमा से सम्बन्धित उत्थान और पतन। निकृष्टता एवं उत्कृष्टता को उत्तेजना देने वाला प्रवृत्ति प्रवाह।
अनुभव बताता है कि आहार में न केवल रस-रक्त का निर्माण करने की क्षमता है वरन् वह चिन्तन के स्तर को भी प्रभावित करता है। यहां चर्चा बुद्धिमता बढ़ाने वाली ब्राह्मी, शतावरी, वच, शंखपुष्पी, गोरखमुण्डी जैसी औषधियों का प्रयोग उपयोग करके मानसिक क्षमता को उत्तेजना देने वाले उपचार की नहीं हो रही है, वरन् यह विचारा जा रहा है कि आहार की क्या विशेषतायें मनुष्य की भाव संवेदनाओं से सम्बन्धित उत्कृष्टता-निकृष्टता को उभारती हैं। इन विशेषताओं का पर्यवेक्षण करने के लिए खाद्य वस्तुओं के रासायनिक संगठन का उतना महत्व नहीं है, जितना कि उनके साथ जुड़े हुए अदृश्य वातावरण एवं प्रभाव का। यह प्रभाव उन व्यक्तियों से सम्बन्धित है, जिनने उसे कमाया, उगाया, पकाया, परोसा है।
व्यक्तियों की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। उनके गुण, कर्म, स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नर-नारायण, नरदेव, नर-पशु नरपिशाच के चार वर्गीकरण पुरातन हैं। उनमें और भी कितनी शाखायें हो सकती हैं। यह विभाजन वर्ग, लिंग-वैभव, शिक्षा व्यवसाय, कौशल आदि से सम्बन्धित नहीं वरन आदर्शवादिता विषयक उत्कृष्टता और निकृष्टता के अनुपात के आधार पर है। कितने ही पशु प्रवृत्ति के पिछड़े मूढ़मति अदूरदर्शी एवं अभ्यस्त आदतों से बेहतर जकड़े होते हैं। इन्हें हेय या हीन ही कह सकते हैं। इन्हीं में कुछ उद्दण्ड, आततायी, निष्ठुर प्रकृति के होते हैं और सदा अनीति ही सोचते तथा कुकृत्य ही करते हैं। सज्जनोचित चिन्तन और व्यवहार तो उनसे यदा-कदा ही बन पड़ता है। इन नर-वानरों और नर-पामरों, नर-पशुओं और नर-पिशाचों से सर्वथा विपरीत एक दूसरा वर्ग वह है, जिनमें से एक को सज्जन दूसरे को उदात्त कह सकते हैं। सज्जन मानवी गरिमा का ध्यान रखते, मर्यादायें पालते और सभ्य सुसंस्कारियों जैसा जीवन जीते हैं। वस्तुतः इन्हें ही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा जा सकता है। इससे भी ऊंचा स्तर उनका है, जो अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार होते हैं। स्वयं ब्राह्मणोचित अपरिग्रही संयमी रीति-नीति अपनाकर क्षमताओं को बड़ी मात्रा में बचा लेते हैं और उन्हें पुण्य–परमार्थ के लिए नियोजित करके असंख्यों का उदार करते रहते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में सन्त और अध्यात्म-भाव में ऋषि देवता, तपस्वी, मनीषी आदि कहते हैं। इस वर्गीकरण से यह पता चलता है कि भाव सम्वेदनाओं एवं स्वभाव आचरण के आधार पर किस प्रकार अनेकानेक विभाग विभाजन मनुष्य के हो सकते हैं।
यह चर्चा इसलिए हो रही है कि आहार पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में यह जाना जा सके किस स्तर के व्यक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में विनिर्मित हुआ आहार किन प्रभाव विशेषताओं से सम्पन्न हो सकता है और उसका उपयोग करने वाले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। शारीरिक पोषण में और प्रभाव खाद्य पदार्थों में पाये जाने वाले रसायनों का होता है, ठीक वैसा ही उदरस्थ करने वाले के मनःसंस्थान पर भावनात्मक प्रभाव उन विशेषताओं का पड़ता है जो आहार के उत्पादन से लेकर परोसने की मध्यवर्ती लम्बी प्रक्रिया के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। इन्हीं व्यक्तियों की भली बुरी विशेषतायें उस आहार के साथ अदृश्य रूप से जुड़ी रहती हैं और खाने वाले को उसी दिशा में मोड़ती-घसीटती हैं।
आहार किस क्षेत्र में किस प्रकृति के लोगों द्वारा बोया-उगाया गया। उसे काटने, साफ करने, पीसने, पकाने में किन-किन के साथ उत्पादन का सम्पर्क सधा। देखभाल तो इस गहराई तक भी की जानी चाहिए, पर इतनी लम्बी दौड़ न सध सके, तो कम से कम इतना तो देखा ही जाना चाहिए कि पकाने वाले-परोसने वाले किस प्रकृति के हैं। जो खाया जा रहा है, वह रासायनिक दृष्टि से सुपाच्य एवं जीवन तत्वों सहित है या नहीं। इसके लिए आहार की अपनी प्रकृति भी होती है। सात्विक से तात्पर्य अमृताशन स्तर के आहार से है। उबले हुए चावल-दाल, दलिया, खिचड़ी जैसे आहार को अमृताशन कहते हैं। शाक-भाजी भी साथ में ही उबाले जा सकते हैं। हलका-सा नमक, अदरक, नींबू जैसे सम्मिश्रण भी स्वाद की दृष्टि से किये जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी न मिलाया जाय, तो अस्वाद व्रत भी निभता है और सात्विकता का अनुपात और भी अधिक बढ़ जाता है। दूध-दलिया, दूध चावल भी अमृताशन वर्ग में आते हैं।
राजसी-तामसी स्तर के वे हैं, जिनमें तलने-भूनने का आश्रय लिया जाता है, चिकनाई, मिठाई तथा मसालों की भरमार की गई हो। इन दिनों दावतों में प्रायः ऐसी वस्तुयें परोसी जाती हैं। कई दिन पूर्व के बनाये बिस्कुट जैसे पदार्थ इसी श्रेणी में आते हैं। उत्तेजक मादक पेय भी तमोगुणी कहे जा सकते हैं। होटलों में जहां एक ही रसोई घर में शाकाहारी, मांसाहारी वस्तुयें पकती हैं, जूते पहने, बिना नहाये, मैले-कुचैले हाथों से पकाते-परोसते हैं। एक के प्रयोग के बाद दूसरे के सामने भी वे ही बर्तन बिना अच्छी तरह धोये-मांजे रख दिये जाते हैं। ऐसी दशा में उनमें किया हुआ भोजन उन कुसंस्कारों में जुड़ जाता है, जो पहले वालों ने उस पात्र के साथ छोड़े थे।
पिछले दिनों रोटी-बेटी की पवित्रता का प्रचलन था। अब उसमें शिथिलता आने लगी है। जाति बिरादरी और और ऊंच-नीच की दृष्टि से तो इस प्रकार के प्रतिबन्धों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु आहार में सात्विकता-सुसंस्कारिता बनी रहे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पकाने-परोसने वाले शारीरिक मानसिक दृष्टि से निरोग तो होने ही चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे कुकर्मी, कुसंस्कारी एवं दुष्ट स्वभाव के न हों। छूत के रोग एक-दूसरे से तक पहुंचते हैं, इसी प्रकार के सम्पर्क से कुसंस्कार भी आक्रमण करते हैं। खान-पान के सम्बन्ध में इन बातों का विशेष ध्यान उन लोगों को रखना चाहिए, जो अपने चित्त-वृत्तियों को उच्चस्तरीय रखना चाहते हैं और चिन्तन में अवांछनीय को घुसने न देने के लिए विशेष रूप से इच्छुक है।
पिप्पलाद ऋषि ने मात्र पीपल के फल खाकर ही निर्वाह किया था। औदुम्बर ऋषि गूलर मात्र लेकर जीवनचर्या चलाते थे। कणाद जंगली घासों से उपलब्ध होने वाले सांवा, मकरा, कोदों, साठी जैसे अनायास ही उत्पन्न होने वाले बीज कणों को समेटकर पेट भरते थे। कन्द-मूल फल पर ऋषियों की उदरपूर्ति होती थी। यह सब अब वन वन प्रदेशों में अनायास उत्पन्न नहीं होता प्रयत्नपूर्वक स्वयं उगाना पड़ता है। अच्छा तो यही है कि अपने एक छोटे खेत में परिवार के लायक अन्न और शाक स्वयं उगायें। इससे परिवार भर को श्रमरत रहने का अवसर मिलेगा। आलस्य से बचने और सृजन चिंतन का अभ्यास बढ़ेगा। जिनके पास खेत नहीं है, वे आंगन बाड़ी, छतबाड़ी, छप्पर बाड़ी की व्यवस्था बनाकर मौसम के अनुरूप शाक-भाजी, उगाने का प्रयत्न करें। छोटे परिवार की शाक-व्यवस्था इतने से भी बन सकती है। बड़ा परिवार हो तो भी इतने के लायक धनिया, पोदीना, अदरक, पालक, सलाद जैसी वस्तुयें आसानी से उगाई जा सकती हैं।
इन दिनों रासायनिक खादें और कीट-नाशक दवाओं की भरमार है। कोल्ड स्टोरों में महीनों तक रखे रहने पर भी आहार की ताजगी चली जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रबन्ध करें कि आहार उत्पादन की दिशा में स्वावलम्बी होने के लिए प्रयत्नशील रहा जाये। महत्व समझने ध्यान जाने और प्रयत्न करने पर मनुष्य अनेक गुत्थियों के समाधान ढूंढ़ निकालता है। तब कोई कारण नहीं है कि परम प्रिय काया आरोग्य जैसी सम्पदा एवं स्वजन-स्नेहियों से भरे परिवार—की महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य-पदार्थों की शुद्धता के लिए कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है।
अपना खेत न हो तो, पड़ौसियों से उसे किराये पर लिया जा सकता है। कुछ अधिक जमीन मिल सके तो आहार उत्पादन में ही गौ-पालन को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। कृषि उपज का अन्न भाग मनुष्य के लिए और चारा पशुओं के लिए एक साथ उत्पन्न होता है। कृषि और पशु पालन का संयोग सुयोग भी है।
इन दिनों बाजार में खरीदने पर दूध के नाम पर जो मिलता है, उसकी जानकारी सभी को है। मिलावट ही नहीं, गन्दगी भी उसमें भरी रहती है। स्वच्छता जब अपने स्वभाव में ही नहीं है, फिर जिसका उपयोग दूसरों को करना है, उसे शुद्धतापूर्वक दुहते, स्वच्छ बरतन में रखने और देर तक रखे रहने पर उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाने की बात कौन सोचे? दूध की आवश्यकता यदि सचमुच ही अनुभव होती है, तो परिस्थितियों को देखते हुए एक कदम और आगे की बात सोचनी चाहिए और गौ-पालन की अपनी व्यवस्था आप करनी चाहिए।
गाय से गोबर, गोबर से भूमि को खाद, खाद से उपज, उपज से, मनुष्य और पशुओं का निर्वाह—यह एक ऐसा चक्र है, जिसे गतिशील रखने में भूमि, पशु और मनुष्य, तीनों की ही भलाई है। इस गतिचक्र को बनाये रहा जाये, तो सरल, सौम्य, सात्विक और सुखी, समृद्ध जीवनचर्या का उपक्रम ठीक प्रकार बना रह सकता है। इसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। सुखी, सन्तुलित सन्तुष्ट और स्वस्थ-समृद्ध जीवनचर्या भी इसी प्रक्रिया में समाहित है। अन्न-शाक की तरह दूध का भी स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान है। कभी दूध बाहर से भी शुद्ध मिल सकता था, पर आज तो समय के प्रभाव से वह सब भी दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसी दशा में तद्विषयक स्वावलम्बन और भी अधिक आवश्यक हो गया है।
आरोग्य से न केवल आहार का वरन् श्रम का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। शारीरिक श्रम की उपेक्षा करने पर कल पुर्जे शिथिल ही नहीं पड़ जाते, वरन् जंग खाये औजार की तरह बेकार भी हो जाते हैं, श्रम को आहार के साथ जोड़ कर एक समग्र स्वास्थ्य श्रृंखला को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आटा-दलिया हाथ की चक्की सी पीसा जाये, धान कूटे जायें, दूध दुहने और मथने का अभ्यास रखा जाये, कुएं से पानी खींचने और कपड़े धोने जैसे घरेलू काम-काजों को अपनाये रहने पर महिलाओं को उपयोगी श्रम करने का अवसर मिलता रह सकता है। बच्चे तक फूल-पौधों से—बछड़ों बैलों के साथ खेलते रह सकते हैं। पक्षियों के साथ आंख-मिचौनी चलती रह सकती है। कैसे सुखद, स्वाभाविक और सन्तोष-उल्लास से भरा-पूरा हो सकता है, यह जीवन क्रम। इस पुरातन परम्परा को यदि नये उत्साह और नई सूझ-बूझ के साथ अपनाया जा सके तो समझना चाहिए कि स्वस्थता और प्रसन्नता के दिन फिर वापस लौट आये।
इस सन्दर्भ में सीखना कुछ नहीं है। जो भुला दिया गया है उसे फिर से स्मरण करना है और जो प्रगतिशीलता के अहंकार में उद्धत स्वेच्छाचार अपना लिया गया है, उसे भुला देना है। यह भूलने और स्मरण करने की विधा ही उस स्वर्णिम युग को वापस ला सकती है, जिसे हम सब उच्छ्वास भरते हुए सतयुग के नाम से स्मरण करते रहते हैं।
आरोग्य मात्र शरीर तक ही सीमित नहीं है। उसकी परिधि मानसिक स्वस्थता तक चली जाती है। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। एक गिरेगा तो दूसरा भी स्थिर न रह सकेगा। इसलिए जब भी सोचना हो, दोनों की सम्मिलित स्वस्थता की बात सोचनी चाहिए। इसके लिए आहार और विहार दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए और ऐसा जीवनक्रम अपनाना चाहिए जिससे इनमें से एक भी टूटने-डगमगाने में न पाये। इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम आहार की उपयुक्तता पर ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि वह पोष्टिक ही नहीं सात्विक स्तर का भी है क्या।