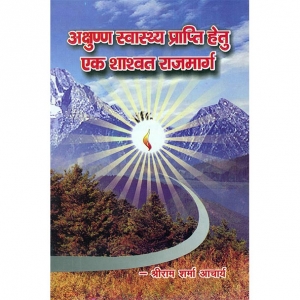अक्षुण्ण स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु एक शाश्वत राजमार्ग 
कुपोषण का मूल कारण नासमझी
समझदारी का सदुपयोग यह है कि उसके सहारे सीधा रास्ता तलाश किया जाय और ऊंचा उठने, आगे बढ़ने में उपलब्ध शक्तियों को नियोजित किया जाय। उसके विपरीत यदि समझदारी कुचक्र रचने लगे, विनाश पर उतरे, उलटे रास्ते चले तो उससे हानि ही हानि है। इससे तो वे नासमझ अच्छे जो कछुए की तरह धीमी चाल चलते, लक्ष्य का ध्यान रखते और उछलने वाले खरगोश से आगे निकलकर बाजी जीतते हैं।
मनुष्य की तुलना में इस दृष्टि से पशु अधिक समझदार हैं जिन्होंने प्रकृति मर्यादाओं को अपनाये रखा है और मनुष्य के नागपाश तथा प्रकृति प्रकोप का सामना करते हुए भी अपना अस्तित्व बनाये रखा है। जो इन साधन रहित परिस्थितियों में भी मात्र अपनी काया, प्रकृति प्रेरणा और कठोर श्रम करने पर सम्भव हो सकने वाली निर्वाह व्यवस्था भर से काम चलाते और सुख-चैन की जिन्दगी जीते हैं। एक मनुष्य है जो विपुल वैभव का अधिष्ठाता होते हुए भी आये दिन ऐसे त्रास सहता है जैसे पुराणों में यमदूतों द्वारा नरक क्षेत्र में पहुंचने पर दिये जाने का उल्लेख है। होना यह चाहिए था कि स्रष्टा के इस सुरम्य उद्यान में मनुष्य शरीरधारी देवोपम स्तर का निर्वाह करता और अपने प्रभाव क्षेत्र को स्वर्ग में अवस्थित नन्दन वन जैसा सुरम्य बनाकर रखता। पर दुर्भाग्य को देखा जाय, ठीक उलटी स्थिति में उसे दिन गुजारने पड़ रहे हैं।
सबसे निकटवर्ती सबसे वफादार, सबसे उपयोगी अपना शरीर है। उसी पर सवारी गांठ कर जीवन की लम्बी मंजिल पूरी की जाती है। इसी वैभव के सहारे इच्छा–अभिलाषाओं को पूर्ण करने का सुयोग मिलता है। जब तक वह सही है तब तक ही शान्तिपूर्वक रहना, विभिन्न प्रकार के रसास्वादन करना तथा प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकना सम्भव होता है। वह गड़बड़ाये तो करते कुछ नहीं बनता। दिन गुजरना तक कठिन पड़ता है। उलटे त्रास सहना पड़ता है। रोते-कलपते समय कटता है और साथी-संबंधियों पर सेवा सहायता करने से लेकर धन व्यय करने तक का भार लदता है।
इतना जानते हुए भी यदि कोई जान बूझकर अपने पैरों कुल्हाड़ी मारे, कांटों पर चले, गड्ढे में गिरे और बर्र के छत्ते में हाथ डाले तो कोई क्या करे? समझदारी का अभाव समझ में आता है। इसके लिए भाग्य-भगवान को दोष देकर भी जी हलका किया जा सकता है किन्तु तब क्या किया जाय जब समझदारी उलटे रास्ते चले? पैर ऊपर करके हाथों के बल, धरती से सिर रगड़ते हुए चलने में विशिष्टता के अहंकार का प्रदर्शन करे।
मनुष्य की गतिविधियों को देखकर ऐसी ही स्थिति का अवलोकन करना पड़ता है। जब अपने परमप्रिय सेवक सम्बन्धी के लिए नासमझी भरी अनीति अपनाते हुए देखा जाता है तब आश्चर्य होता है असमंजस पड़ता है कि मनुष्य की समझदारी को सराहा जाय या उसकी उलटे पैरों चलने लौटने की विडम्बना को मूर्खतापूर्ण कहकर कोसा जाय।
शरीर के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसे उलट-पुलट कर देखा जाय तो एक शब्द में विचित्र ही कहा जा सकता है। शरीर के साथ शत्रुता निवाही जाय, उसे तोड़-फोड़कर बर्बाद किया जाय ऐसा भी किसी का मन नहीं दीखता यदि ऐसी बात रही होती तो वस्त्र आभूषणों से, श्रृंगार प्रसाधनों से क्यों सजाया जाता? केश-विन्यास बनाने जैसे अनेकों कामों में कितना समय लगता है? सजधज में कितना धन व्यय होता है? वाहनों, सेवकों द्वारा उसके लिए कितनी सुविधायें प्रदान की जाती हैं। विनोद के कितने ही साधन जुटाये जाते हैं? पोषक आहार लेने का भी ध्यान रहता है। इन सब बातों को देखते हुए यह कैसे कहा जाय कि अपनी काया के प्रति किसी का मन शत्रुता निवाहने का है और उसे बर्बाद कर देने का इरादा बन गया है।
दूसरी ओर दृष्टि डालने से जो दृश्य सामने आता है उसे देखते हुए यह मानने को भी जी नहीं करता कि शरीर को मित्र माना गया है और उसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा प्रति का वैसा ध्यान रखा गया है जैसा कि किसी समझदार को रखना चाहिए था। एक-एक करके पर्यवेक्षण करना हो तो सर्वप्रथम दृष्टि आहार पर जानी चाहिए क्योंकि इसी ईंधन के सहारे यह भट्टी गरम रहती है और इसी पर पकने वाली खिचड़ी के सहारे जीवन की गाड़ी चलती है। रस-रक्त का तेल-पानी ही है जिसके बलबूते यह मोटर दौड़ती है। इस सन्दर्भ में असावधानी बरती जाय, उलटी नीति अपनाई जाय तो स्पष्ट है कि उस आधार को विषाक्त होना पड़ेगा जिसे आरोग्य की आधारशिला कह सकते हैं। अनुपयुक्त आहार करते रहने पर भी कोई किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकेगा? इस तथ्य को समझने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी स्पष्ट है कि आहार के सम्बन्ध में वह ढर्रा अपनाया गया है जिसके रहते निरोग रह सकने की बात सोची भी नहीं जा सकती। आश्चर्य यह है कि दुष्परिणाम भुगतने में इतनी देरी क्यों होती रहती है। प्रकृति को कठोर अनुशासन की अधिष्ठात्री कहा जाता है फिर भी वह मनुष्य के साथ धीमी और थोड़ी प्रताड़ना देने की उदारता क्यों कर दिखा पाती है।
अभ्यस्त आहार का निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाय तो प्रतीत होता है कि उसे निर्जीव और विषाक्त बनाने में कोई कमी नहीं रहने दी गई है। स्वादिष्ट के ध्रुव केन्द्र समझे जाने वाले नमक पर दृष्टि डाली जाय तो प्रतीत होता है कि यह मनुष्य के आहार में सम्मिलित होने योग्य स्थिति में किसी भी प्रकार नहीं है। रासायनिक विश्लेषण करने पर वह ‘सोडियम क्लोराइड’ नामक विष है। जिसकी पोषण में सहायता दे सकने जैसी स्थिति तनिक भी नहीं है। जो नमक शरीर में घुलते और पोषण प्रदान करते हैं वे अन्न, शाक, फल आदि खाद्य पदार्थों में प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं। वे ही पचते और चपते भी हैं। इस प्रकार शरीर की लवण आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका समुचित अनुपात उन खाद्य पदार्थों में संजोया है जो खाने के काम आते हैं। उनका अन्याय रासायनिक पदार्थों के साथ ऐसा समन्वय भी रहता है जिससे उनके पचने में सुविधा रहे। आवश्यक नहीं कि उन उपयोगी लवणों का स्वाद खारा ही रहे। ‘फ्रूट साल्ट’ खारे कहां होते हैं?
मनुष्य है जिसे खारी नमक के बिना एक ग्रास गले उतारना कठिन पड़ता है। दाल, शाक, चटनी, अचार कुछ क्यों न हो—हरेक में चटकीला नमक रहना चाहिए। इसके बिना जायका ही क्या? यह बुरी आदत जान-बूझकर डाली गई है। संसार के अनेक क्षेत्र इन दिनों भी ऐसे हैं जहां खारी नमक का उपयोग प्रायः नहीं ही होता है। देखा देखी प्रचलन हुआ है तो उसकी मात्रा नगण्य जितनी रखी गई है। इसका प्रतिफल प्रत्यक्ष है। उन क्षेत्र में सभ्य जगत् की प्राणप्रिय बीमारियां अभी भी पहुंच नहीं पाई हैं।
अन्य मसालों के सम्बन्ध में भी यही बात है। जीरा, धनियां, हल्दी जैसे मसालों को तो किसी प्रकार सहन भी किया जा सकता है। किन्तु मिर्च, लौंग, हींग, तेजपात जैसे गरम मसाले तो ऐसे हैं जिन्हें एक प्रकार का तेजाब ही कहना चाहिए। वे जलाने गलाने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम कर ही नहीं पाते। हन्टर मार-मार कर दौड़ाने जैसी उत्तेजना देकर पेट के साथ अत्याचार ही करते रहते हैं। अधिक खाये को जल्दी पचाने की बात आमतौर से मसालों का लाभ बताते हुए कही जाती हैं। पर वस्तुतः वे निर्दय चाबुकमार की गतिविधियां ही अपनाते हैं और नशे की तरह आदत में सम्मिलित हो जाने के बाद यह विवशता उत्पन्न करते हैं कि उनके बिना गाड़ी धकेगी ही नहीं।
मिर्च-मसालों के आवेश में मनुष्य अधिक खा जाता है। जो अभक्ष्य थे उन्हें भी निगल जाता है। अवांछनीय तत्वों को शरीर में प्रवेश देने पर कोई अपनी चतुरता की डींग क्यों न हांके, पाक विद्या के निष्णात अपने कौशल की शेखी कितनी ही क्यों न बघारें—वास्तविकता यह है कि उस चतुरता के सहारे आरोग्य के सर्वनाश का ही द्वार खुलता है। लाड़-चाव में प्रियजनों को स्वादिष्ट व्यंजन बना-बनाकर खिलाना और अधिक खाने का आकर्षण या दबाव प्रस्तुत करना वस्तुतः ऐसी शत्रुता है जिसे लोक व्यवहार में मित्रता, शुभेच्छा का प्रदर्शन समझा जाने लगा है।
न जाने यह समझदारी कहां से मनुष्य पर चढ़ दौड़ी की अधिक खाने से अधिक बल मिलता है, जबकि बात तथ्य के सर्वथा विपरीत है। पेट की बनावट ही ऐसी है कि यदि वह आधा भरा हो तो पाचन का ठीक प्रबन्ध कर सकता है। हांडी खाली रहे तो ही उफनने-उबलने की गुंजायश रहने पर ठीक प्रकार पकेगी। मयानी में दही बिलोने के कारण जो हलचल होती है उसके लिए जगह छोड़नी पड़ती है। यदि हांडी खचाखच भरी हो तो पकने की प्रक्रिया कैसे पूरी हो? मथनी को गरदन तक भर दिया गया हो तो बिलोने पर जो उथल-पुथल होती है उसके लिए स्थान कैसे मिले?
पेट के खाली रहने पर ही पाचन की गुंजायश रहती है। सीमित रस स्राव होने पर सीमित मात्रा का आहार ही पचता है। गले तक बोझा भर लेने पर यह आशा छोड़ ही देनी चाहिए कि वह ठीक प्रकार पचेगा और उपयुक्त पोषण प्रदान कर सकेगा। मिर्च-मसाले इस व्यवस्था को बुरी तरह बिगाड़ देते हैं। उनसे दुहरी हानि है। एक यह कि वे अपनी उत्तेजक विषाक्तता के कारण पाचन तन्त्र की तोड़ फोड़ करते हैं दूसरी यह कि उस लालच में अधिक मात्रा में खाते जाने पर भी हाथ रुकता नहीं। फलतः पेट को अकारण अत्यधिक श्रम करने पर भी पोषण के नाम पर खाली हाथ रहना पड़ता है। अपच उत्पन्न होने पर बीमारियों का आक्रमण दौड़ पड़ता है सो अलग। इस प्रकार स्वादिष्ट के नाम पर नमक और मसालों का उपयोग होता है। उनसे लाभ जैसा तो कुछ मिलता नहीं। शरीर पर विपत्ति लदती है।
मिर्च मसालों जैसी स्थिति ही चिकनाई-मिठाई की है। तेल घी को अलग से निकालकर खाने से वे तत्व अलग हो जाते हैं जो चिकनाई को पचाने में काम आते हैं। तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि को चबाकर या पीस कर उपयोग किया जाय तो वे उचित मात्रा में होने पर पोषण का प्रयोजन पूरा करेंगे। तेल निकालने पर उसे पचाने वाले तत्व खली में निकल जाते हैं और वह चिकनाई अत्यधिक गरिष्ठ हो जाती है। घी खाने की अपेक्षा दूध दही लेना गनीमत है। वैसे जितनी चिकनाई की शरीर को आवश्यकता है उतनी सन्तुलित आहार में सहज ही मिल जाती है। अन्न, दाल आदि में भी चिकनाई होती है। अलग से उसे लेना आवश्यक नहीं है पर यदि लेने का मन ही हो तो उसे उन बीजों के रूप में ही लेना चाहिए जिनमें तेल ही नहीं उसको पचाने वाले तत्वों का भी उपयुक्त अनुपात रहता है।
शक्कर के सम्बन्ध में भी यही बात है। अन्न मुंह में पिसता है तो जीभ से निकलने वाले रस ही उसे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पेट में पहुंचते-पहुंचते वह उपयुक्त मात्रा में शक्कर से भरा-पूरा होता है। फिर सामान्य खाद्य पदार्थों में भी शक्कर का समुचित अनुपात रहता है। उसे अलग से खाने की कोई आवश्यकता नहीं। मीठे फलों में उसका अनुपात पर्याप्त होता है। प्रायः सभी फल मीठे होते हैं। खजूर, अंजीर, दाख आदि में तो उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। शहद की भी प्रशंसा है। यों चीकू से लेकर चुकन्दर तक में उसकी पर्याप्त मात्रा रहती है। मन चले तो गन्ना भी चूसा जा सकता है। शक्कर प्राप्त करने की इतनी ही मर्यादा है। चरम सीमा तक पहुंचा हो तो बिना पाउडर के शोधा गया गुड़ या राब तक आगे बढ़ा जा सकता है। सफेद चीनी तो सफेद विष कही गई है। कैल्शियम निकल जाने पर तो वह दांत मसूड़े, अस्ति पिंजर आदि सभी को गलाती है। मधुमेह, रक्तचाप, यकृत रोग, पेट के कीड़े जैसे रोग उत्पन्न करने में तो ही करामात काम करती है। यदि सफेद चीनी का उपयोग आहार से हटा दिया जाय तो विषय भक्षण चटोरपन, अपव्यय एवं अधिक खाने जैसे अनेक अभिशापों से सहज छुटकारा मिल सकता है।
मनुष्य की शरीर संरचना पूर्ण शाकाहारी जैसी है। वह वानर प्रजाति है। इस वर्ग समुदाय के लिए मांसाहार तनिक भी नहीं। दांत, आंत जैसे अवयवों की बनावट ऐसी है नहीं जो मांस पचा सके। तल भूलकर के लोग वांस और आक के पत्ते जैसी वस्तुओं के व्यंजन बना लेते हैं। इसका तात्पर्य यह तो नहीं हुआ कि वे मनुष्य के आहार सूची में सम्मिलित होनी चाहिए। मांस मनुष्य के लिए न तो सुपाच्य है और न उपयुक्त। वह मात्र हिंस्र प्राणियों के लिए ही उपयोगी है मनुष्य में सहज स्वभाव पाई जाने वाली दया भावना भी इसकी आज्ञा नहीं देती कि वह शरीर और मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले मांसाहार पर उतरे जबकि शाकाहारी पदार्थों का बाहुल्य प्रकृति ने उसके लिए पहले से ही संजोकर रख दिया गया है।
आहार क्षेत्र में घुसी हुई अवांछनीयताओं में से कुछ पर ऊपर की पंक्तियों में प्रकाश डाला गया है। भूनने तलने की समूची प्रक्रिया ही ऐसी है जिसे हर दृष्टि से अबुद्धिमत्तापूर्ण ही कहा जायगा। व्यंजनों का प्रचलन अपने समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। थाली में अनेकों कटारियों का सजाया जाना अनेक स्वादों की भरमार होना—ऐसी नासमझी है जिसके कारण चटोरेपन की दाद खुजाने जैसी राहत भले ही मिलती हो पर परिणामतः उससे हानि ही हानि है। हित साधन जैसी बुद्धिमत्ता की उसमें कहीं झांकी तक नहीं होती।
गलत रास्ते पर चलने की जानकारी मिलते ही यात्री वापिस लौट पड़ते हैं, जो भूल का परिमार्जन सही रास्ता अपनाकर करते हैं। उपरोक्त अभ्यस्त कुटेवों को यदि आहार प्रक्रिया में से हटाया जा सके तो यह भूल सुधार का एक उत्साहवर्धक प्रयोग होगा। उसका सत्परिणाम हाथोंहाथ—स्वास्थ्य में आशाजनक परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर होगा। वस्तुतः सारी पोषण समस्याओं की कारण वह नासमझी है जो मनुष्यों के मन मस्तिष्कों में जड़ जमाये बैठी है। जब तक अज्ञानान्धकार नहीं दूर होगा अवांछनीयतायें आहार में प्रवेश कर बीमारियां बढ़ाती रहेंगी, बाहरी उपचार निरर्थक ही रहेंगे।