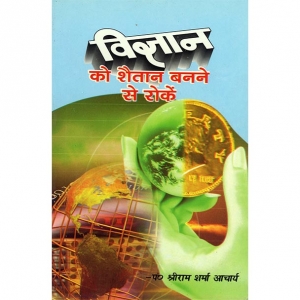विज्ञान को शैतान बनने से रोकें 
मनुष्य पूरी तरह मशीन न बने
Read Scan Version
प्रकृति की व्यवस्थायें इतनी सर्वांगपूर्ण हैं कि उसे ही परमात्मा के रूप में मान लिया जाय तो कुछ अनुचित नहीं होगा। शिशु जन्म से पूर्व मां के स्तनों में ठीक उस नन्हें बालक की प्रकृति के अनुरूप दूध की व्यवस्था, हर प्राणी के अनुरूप स्वतंत्र खाद्य व्यवस्था बनाकर वनस्पति जगत में सन्तुलन बनाये रखने की तरह दुर्बुद्धि को ठिकाने लगाने वाली उसकी कठोर नियम व्यवस्था भी सुविदित है। जिन प्राणियों में प्रजनन बढ़ता है उनका सर्वनाश वह हारी-बीमारियों के रूप में करती रहती है। प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग ही अकाल और अभाव के रूप में दिखाई देता है। मानवीय स्वभाव की कृत्रिमतायें और प्रकृति के बहिष्कार का दण्ड शारीरिक आधि-व्याधि के रूप में भुगतना पड़ता है। यह नियम व्यवस्थायें इस बात की प्रतीक हैं कि प्रकृति में विवेकपूर्ण आचरण की सम्वेदना पूरी तरह विद्यमान है उसकी व्यक्तिगत उल्लंघन, व्यक्तिगत दंड के रूप में तथा सामूहिक उल्लंघन, सामूहिक दंड के रूप में हर किसी को भुगतना पड़ता है इस नियम व्यवस्था से सृष्टि का कोई भी प्राण बच नहीं सकता।
प्रकृति ने उतने साधन पहले से ही जुटाकर रखे हैं जिनका यथोचित और उपयोगी मात्रा में उपयोग किया जाता रहे तो हर व्यक्ति सुखी जीवन, नीरोगिता का जीवन, पारस्परिक शान्ति और सद्भाव का जीवन जी सकता है, पर सब इन्द्रियों की सामर्थ्य से बहुत अधिक और असीम उपभोग की तृष्णा बढ़ी तो स्वाभाविक था मनुष्य कोई ऐसा रास्ता अपनाता जिसमें कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकता। इस महत्वाकांक्षा और अनियन्त्रित भोग बुद्धि ने अभियांत्रिकी को जन्म दिया। हाथ का काम, पैर का काम, यहां तक कि बुद्धि का काम भी मशीनों ने ले लिया। हाथ-पांव चलते रहें इसके लिए परमात्मा ने मनुष्य में इच्छायें पैदा कीं, पर उसका यह उद्देश्य कभी नहीं रहा कि इच्छायें उसकी साध्य बन जायें। यही भूल हुई जिससे मनुष्य स्वयं मशीन बनता जा रहा है। हर काम मशीन करे, तो फिर हाथ, पांवों में जंग लगना स्वाभाविक ही है, बीमारियां बढ़नी स्वाभाविक हैं, ‘‘खाली दिमाग शैतान का घर’’ की उक्ति के अनुसार बौद्धिक भ्रष्टाचार, पाप और पतन की सम्भावनाओं का विकास स्वाभाविक ही था सो इन दिनों वही हो भी रहा है। यन्त्रीकरण के दुष्परिणाम भुगत रहे हैं सो अलग आज तो यह साधन ही सामूहिक सर्वनाश के कारण बन बैठे हैं।
पैदल चलना भी आवश्यक
आये दिन वायुयान दुर्घटनाओं रेलों की भिड़न्त और उससे सैकड़ों लोगों की दुर्घटनायें समाचार पत्रों में आती रहती हैं, उन्हें भी आकस्मिक व अपवाद के रूप में ही माना जाता है। आज जब कि संसार की जनसंख्या भीषण रूप से बढ़ रही है सम्भव है इन दुर्घटनाओं का मूल्य न आंका जाता हो, पर यातायात के यान्त्रिक साधनों की वृद्धि ने जन-जीवन को दुर्घटनाओं से कितना भयाक्रान्त कर दिया है इसकी कल्पना भी कम दुःखद नहीं है। यह रोग चूंकि अभी भारतवर्ष में अधिक नहीं फैला इसलिए उधर ध्यान कम जाता है, पर इस दृष्टि से पश्चिमी देशों का निरीक्षण करें तो यही कहना पड़ेगा—मनुष्य यातायात में इतनी शीघ्रता न कर पैदल चलने में ही राजी रहता तो कहीं अधिक नफे में रहता।
अमरीका में रास्तों पर चलने वाले 10 में 17 व्यक्ति मोटर, ठेलों द्वारा कुचल दिये जाते हैं, इंग्लैंड में प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत सड़कों पर चलने वाले लोग घर के बजाय स्वर्ग पहुंचा दिये जाते हैं। इटली में कारों की संख्या कम है 200 में से 9 के पास ही कारें होती हैं तो भी यह कम करें ही 56 प्रतिशत पथिकों को कुचल डालती हैं और जापान जिसका औसत इटली से भी कम है प्रतिवर्ष 100000 यात्रियों में से 402.2 आदमियों को पीस डालता है। इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करने पर पता चला कि संसार में आज यातायात दुर्घटनाओं से उतने लोग मरते हैं जितने संक्रामक बीमारियों से भी नहीं मरते।
पैदल चलने में शरीर की नस-नस हिल अवश्य जाती है, पर उससे शरीर में कितनी शक्ति आती है यह भी किसी से छिपा नहीं। एक मील चलने से शरीर को जो व्यायाम करना पड़ता है उससे मनुष्य को 1 दिन के लिए अतिरिक्त शक्ति मिलती है और 1 दिन की आयु बढ़ जाती है। प्राचीनकाल में लोग लम्बी-लम्बी यात्रायें बहुत थोड़े समय में किया करते थे उनमें इतनी शक्ति और स्फूर्ति बनी रहती थी जब कि आज मोटरों और कारों पर चलने वाले लोग आराम से यात्रायें करने पर भी घर वापिस आने पर हारे, थके, टूटे और बीमार से लगने लगते हैं। प्राचीनकाल में तीर्थयात्राओं और परिक्रमाओं का विधान था, उसमें जहां शुद्ध और सुसंस्कृत वातावरण का लाभ लेने का भाव था वहां हमेशा घरों में बैठे रहने के आलस्य को पैदल यात्राओं द्वारा भगाना भी उद्देश्य था। इन यात्राओं से परिक्रमाओं से लोग भरपूर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते थे।
मोटर हों चाहे रेलें उनका धुआं और गैस यात्रियों के मस्तिष्क पर बुरा असर डालती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डा. रौस.ए. मैकफारलैण्ड का कथन है कि मनुष्य को नियमित रूप से स्वस्थ और ताजा रखने के लिए 18 से 50 फुट प्रति सेकेंड की गति से चलती हुई 1 घन मीटर ताजी हवा की आवश्यकता होती है इसी प्रकार वायु में नमी की 15 प्रतिशत से कमी भी स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर बुरा असर डालती है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सामूहिक अपान और मुंह से निकाली हुई दूषित वायु मोनो ऑक्साइड पैदा करती है जिससे देखने में आराम से यात्रा करने वाले यात्री की आंख, कान, मस्तिष्क और रक्त में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यह विकार जहां यात्रियों के लिए स्वास्थ्य-घातक होते हैं वहां ड्राइवरों के लिए ज्ञान नाशक। उनके मस्तिष्क के तन्तु और मांस-पेशियां नियन्त्रण में रहना छोड़ देती हैं दुर्घटनायें उसी का प्रतिफल होती हैं आज सारा योरोप उसके निश्चित दुष्परिणाम भुगत रहा है।
इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन?
यह कहना चाहिए कि आज योरोप में यात्रा करना उतना ही जोखिम भरा हो गया है जितना कि तूफानी समुद्र में टूटी हुई नाव लेकर चलना। स्वीडन में 1 लाख वाहन प्रतिवर्ष 76.1 आदमियों को रौंद डालते हैं, अमेरिका में अनेक सुरक्षा साधनों के बावजूद 52.6 न्यूजीलैण्ड में, 53.8 तो डेनमार्क के 1 लाख रजिस्टर्ड वाहन 101.8 यात्रियों को मार डालते हैं। फ्रांस उससे भी आगे है वह अपनी इतनी मोटरों, कारों और ठेलों द्वारा 112.9 व्यक्तियों को पीस डालता है तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की गाड़ियां क्रमशः 153 और 159.8 व्यक्तियों को जिन्दा चबा जाती हैं। यह अकाल मृत आत्मायें, आकाश और वातावरण में हा-हाकार करती घूमती होंगी तो उससे मनुष्य जाति का सूक्ष्म अन्तःकरण कितना अशान्त होता होगा उसकी कल्पना करना भी कठिन है।
सारा संसार घण्टे भर की यात्रा की सीमा में आ जाय उससे लाभ कुछ नहीं हानियां अपार हैं। इसलिए यातायात के साधनों में वृद्धि द्वारा सारे संसार को एक बिन्दु पर ला देने का तर्क कोरी मूर्खता है। जब यह साधन नहीं थे इतिहास बताता है कि तब भी सारा संसार इतने ही समीप था। समीपता विचारों, सिद्धान्तों और मानवीय आदर्शों की ही अच्छी हो सकती है, उसके दूसरे माध्यम हैं गन्दगी बढ़ाने वाले शरीरों की समीपता से जो विकास बढ़ने चाहिये आज संसार में वही बढ़ रहे हैं। अतएव इन साधनों के विकास के प्रयत्नों का अच्छा कदापि नहीं कहा जा सकता।
आज सब कुछ इससे उल्टा हो रहा है। योरोप में प्रतिवर्ष 5000 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं और लगभग 1 लाख दुर्घटनाओं के शिकार होकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं फिर भी प्रयत्न यह हो रहे हैं कि यहां अभी 200 व्यक्तियों पर 25 मोटरों का औसत है वहां जल्दी ही 200 व्यक्तियों पर 50 और 75 का औसत हो जाये। यदि विकास की गति इसी तरह बढ़ती गई तो एक दिन वह भी आ सकता है जब न तो पैदल चलने के लिए पगडंडियां रह जायेंगी और न ही पैदल यात्री। तब लोग अपने आप ही दुर्घटनाओं के शिकार होकर मर जाया करेंगे। आखिर यातायात के यह कृत्रिम साधन बढ़ेंगे तो दुर्घटनायें और मृत्यु दरें भी 79 व 37 प्रतिशत से शत प्रतिशत होंगी ही। तब साहित्य भी पैदल चलने के लाभों के स्थान पर यातायात की दुर्घटनाओं का ही लिखा जाया करेगा जो इन पंक्तियों से भयंकर ही होगा। उस विभीषिका से बचाव अभी हो सकता है।
भौतिक प्रगति आत्मिक अवनति
यह बात केवल यातायात तक ही सीमित नहीं। आज के नागरिक की दिनचर्या, रहन-सहन और आदतें देखकर उसकी जो तस्वीर बनती है वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य का जीवन भी एक यन्त्र की तरह हो गया है। पाषाण, लौह और ताम्रयुगीन विभाजनों के साथ वर्तमान सन्दर्भों को देखा जाय तो इसे निश्चित ही यन्त्र युग कहना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन और यान्त्रिक उपकरण परस्पर इतने घनिष्ठ हो गये हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से विलग कर पाना ही असम्भव है। उस क्षण की स्थिति को कल्पनांकित ही नहीं किया जा सकता, जब कि मनुष्य का जीवन यन्त्रों की सुविधा से एकदम रहित हो जाय। मिल कपड़े बनाते हैं, कारखानों में खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, साबुन, तेल, ईंधन आदि सब किसी न किसी रूप में मशीनों से सम्बद्ध मिलेंगे। यहां तक कि जिस रोशनी का हम रात दिन उपयोग करते हैं वह भी रात दिन मशीनों द्वारा ही पैदा होती है और हम तक पहुंचाई जाती है।
हम जिन परिस्थितियों, वातावरणों तथा वस्तुओं के संसर्ग में रहते हैं, उनका हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारा उन पर। मनुष्य से समाज बनता है और समाज मनुष्य को बनाता है। मनुष्य अपने आस-पास के वातावरण से प्रभावित होता है और वातावरण मनुष्य से प्रभावित होता है। प्रभाव पड़ने या पैदा होने की यह प्रक्रिया दोनों ओर से होती है एकांगी कभी नहीं। लेकिन यन्त्रों के सम्बन्ध में कुछ ओर ही सचाई है। सिलाई की मशीन पांव चलाने से चलती है और पांव रोक देने पर बन्द हो जाती है। बाद में वह कोई गति नहीं करती, परन्तु दिन-रात सिलाई मशीन पर बैठने वालों के पांव कभी-कभी अपने आप भी चलने लगते हैं। यह आदतन प्रभाव है।
आदतन प्रभाव की तरह ही मनुष्य भावनाओं से भी प्रभावित होता है और आजकल ‘यान्त्रिक-सभ्यता’ की समीक्षा करते समय इसी भावनात्मक प्रभाव की चर्चा की जाती है। हालांकि संसर्ग के अतिरिक्त इसके और भी कई कारण हैं। इसी तथ्य की ओर इशारा करते हुए प्रसिद्ध विचारक नीत्शे ने कहा था—‘‘यन्त्र जितनी तीव्रता से प्रगति कर रहा है उसी अनुपात से मनुष्य की धर्म सम्वेदना का ह्रास हो रहा है। समस्त भौतिक सुविधाओं से सम्पन्न हो जाने पर भी मनुष्य इतना आत्म-विपन्न हो रहा है कि बीसवीं शती के अन्त तक वह एकदम खोखला हो जायेगा और भयंकर रूप से दुःखी रहने लगेगा।’’
इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक आधुनिक विचारक का कथन है कि—‘‘आज के युग में जीने वाले व्यक्ति की स्थिति विचित्र कम और शोचनीय अधिक है। समस्त मानवीय सम्बन्ध अब केवल वित्तीय स्तर पर बनते हैं अन्य सभी माध्यमों को या तो नगण्य घोषित कर दिया गया है अथवा फिर यान्त्रिकता से जकड़े हुए नये समाज में वे किसी अज्ञात प्रक्रिया द्वारा स्वतः डूबते जाते हैं।’’ चूंकि मनुष्य समाज का एक अंग है और इस नाते उसे दूसरे अन्य अंगों के सम्पर्क में आना पड़ता है। मानवता का तकाजा तो यह है कि हम अपने पड़ौसियों के दुःख-सुख में काम आयें, उनकी खैर-खबर रखें और कुशलक्षेम से अवगत रहने के साथ-साथ समय-समय पर काम भी आयें। परन्तु पड़ौसियों के प्रति यह आत्मीयता का भाव धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानगरों की स्थिति तो यह है कि वहां रहने वाला एक व्यक्ति अपने पड़ौसी के दुःख दर्द में साथ देने के स्थान पर उसे जानता तक भी नहीं शहरों और कस्बों के नागरिकों को भी अपनी समस्याओं से कम ही फुरसत मिल पाती है और इस फुरसत को पड़ौसियों से मेल-जोल बनाने के स्थान पर सिनेमा देखने या सैर करने में गुजारना अधिक अच्छा समझते हैं।
पड़ौसियों से कटे रहने तक की ही बात सीमित रहती तो इतनी शोचनीय स्थिति नहीं आती। आश्चर्य तो तब होता है जब लोगों को अपने रिश्तेदारों और सम्बन्धियों से सम्पर्क रखने का भी समय नहीं मिलता। यही नहीं आदमी अपने बीमार पत्नी के पास बैठने की अपेक्षा दिन भर की थकान उतारने के लिए रेडियो सुनना और घूमने निकल जाना अधिक अच्छा समझता है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई में क्या स्थिति है—इससे अनभिज्ञ रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने शहर में रहने वाले मित्रों और सम्बन्धियों के घर न जाये ही महीनों बीत चुके हैं। अर्थात् मनुष्य समाज में रहता तो है अवश्य, पर समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं—या तो वह अनभिज्ञ है अथवा जान-बूझकर उनकी उपेक्षा करता है।
इतना एकाकीपन होने के बावजूद भी मनुष्य आर्थिक दृष्टि से किसी से सम्पर्क सूत्र कायम करने में चूकना नहीं चाहता। कारण कि यन्त्रों की बाढ़ ने मनुष्य का श्रम हल्का किया है और उसकी सुविधाएं बढ़ाई हैं। इसलिए उपभोग सामग्रियों से बाजार भरे हैं। जो समर्थ हैं, वे उन्हें खरीद सकते हैं तथा उनका उपभोग कर सकते हैं। इस कारण असमर्थ और विपन्न व्यक्तियों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट होता है तथा वे भी उनका वैसा ही उपयोग करने के लिए ललक उठते हैं। बेशक उन्हें खरीदने के लिए अतिरिक्त आर्थिक साधन चाहिए। इस समर्थता और असमर्थता ने सम्पन्नता को ही प्रतिष्ठा का बिन्दु बना दिया है। जिसे हर कोई बींधना चाहता है और उसे बींधने में इस कदर लवलीन है कि उसे अपने आस-पास की चीजें भी नहीं दिखाई देतीं।
यान्त्रिक संसर्ग का जहां तक प्रश्न है मशीनी वातावरण में रहने का अपना एक अलग प्रभाव है। लेकिन उससे भी अधिक बुरी तरह प्रभावित और आत्म-विपन्न कर देने वाली स्थिति, बदलते दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई है। जिसने वित्तीय—दशा को ही सर्व प्रधान बना दिया और उसे पूरा करने के लिए मनुष्य इतना मदमत्त होकर दौड़ने लगा कि एकाकीपन, संत्रास, आत्म-विपन्नता, स्वकेन्द्रित मनोवृत्तियां, कुण्ठाएं और विक्षेप उसे चारों ओर से छेदने लगे हैं। मशीनों के संसर्ग का एक व्यवस्थित कार्य-क्रम है, जो सुखी जीवन की एक निश्चित गारंटी है। परन्तु उसके बावजूद और-और कारण जो यान्त्रिक सभ्यता को दोषों से विषाक्त करते हैं मनुष्य को तनावग्रस्त तथा असुरक्षित बनाते हैं।
अब से 25-50 साल पहले युवकों के सामने जीवन में प्रवेश करने का यह एक रेडीमेड तरीका था कि पढ़ना-लिखना और डिग्री प्राप्त करना तथा उसके बाद नौकरी से लग जाना या शिक्षा प्राप्त करना। नौकरी धन्धे से लगने और परिवार बस जाने के बाद भी युवक को परिवार का आर्थिक संरक्षण मिलता रहता था। इसका एक कारण तो यह था कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी। जिसमें सभी सदस्यों के हित परस्पर जुड़े हुए थे तथा प्रत्येक एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों का अनुभव करते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और एकाकी परिवार अधूरी-अधकचरी स्थिति में जीते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आशा बांधे रहते हैं। अपने माता-पिता और सहोदर भाई-बहिनों से सिकुड़ कर मानवी गतिविधियों का केन्द्र पत्नी, बच्चे और स्वयं तक ही सीमित हो गया है। जो संयुक्त परिवार किसी प्रकार टूटने से बचे हुए हैं, जिनके सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कुछ दायित्व अनुभव करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सजग रहते हैं, वे भी नौकरी और रोजगार करने के लिए बिखरे पड़े हैं। कहने का अर्थ यह कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने के चक्कर में हम और अधिक दीन-हीन व एकाकी बनते जा रहे है। यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग अपने माता-पिता और सहोदर भाई-बहिनों के लिए ही कुछ करना व्यर्थ समझते हों वे पड़ौसियों और मित्रों के लिए कुछ करने की क्या सोचेंगे?
अकेलेपन का यह मानसिक प्रभाव नगरीय लोगों में अधिकांशतः है। इसकी तुलना सौ वर्ष पुराने समाज से करते हुए लिखा गया है—‘‘उन्नीसवीं सदी का मनुष्य अपनी आत्म सम्पन्नता के बल पर ही अनेक दुःख झेलकर भी मानवीयता से भ्रष्ट नहीं हो पाता था और उसकी इस आत्म-सम्पन्नता के पीछे संयुक्त परिवार प्रथा, धर्म और संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ था। जब कि बीसवीं सदी का मनुष्य इतना बर्हिप्रविष्ट हो गया है कि सामान्यतया स्वयं को नगण्य व एकाकी मानता हुआ किसी भी क्षण अपने आपको दूसरों के हाथों में छोड़ देने के लिए विवश हो जाता है या मजबूरन अपने को तैयार करता है।’’
यान्त्रिक सभ्यता में मनुष्य की दृष्टि का केन्द्र बिन्दु बदला है और उसने मानवीयता के स्थान पर आर्थिकता को व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा माना है। वही उसका अपना जीवन भी एकरस और उसके कारण विद्रोही बना है। हाल ही में पिछले वर्षों ब्राक्स में एक अद्भुत घटना घटी। एक बस ड्राइवर अपनी बस समेत अनायास लापता हो गया। तीन-चार दिन बाद वह बस समेत फ्लोरिडा में पकड़ा गया। इस बीच अखबारों में वह बड़ी चर्चा का विषय बन गया। बस कम्पनी के मालिकों ने जब उससे भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछले सात वर्षों से वह एक ही रूट पर बस चलाते-चलाते और उन्हीं स्थानों पर बार-बार बस रोकते-रोकते बुरी तरह बोर हो गया है। परिवर्तन के लिए ही उसे पलोरिडा आने का निर्णय लेना पड़ा।
जैसा कि कहा जा चुका है कि मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा आज अधिक सुनिश्चित और व्यवस्थित कार्य-क्रम है। परन्तु उसकी उबाऊ एकरसता ने मनुष्य की चेतना को एकरस बना दिया है और वह इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये एकदम से तैयार नहीं है। इस उबाऊ एकरसता के कारण वह बोरियत अनुभव करता है और उसे तोड़ देने के लिए स्वच्छन्दता, उन्मुक्तता और हिप्पीवाद की अनेकानेक भ्रान्त धाराओं में वह निकलता चाहता है। यन्त्र जिस प्रकार एक ही गति और लय में चलता है उसी प्रकार मनुष्य भी एक ही स्थिति को बार-बार भोगने के लिये अपने आपको विवश अनुभव करता है। कहने का अर्थ यह है कि वह अपने आपको कोल्हू के बैल वाली स्थिति में पाता है, जिसे उसकी प्रवाहमान गतिशील चेतना किसी भी दशा में भोगने को तैयार नहीं है। एक अर्थ शास्त्री के शब्दों में मनुष्य की चेतना ह्रासमान उपयोगिता की भांति सम्वेदना शून्य बनती जा रही है। वह व्यक्ति को इस सीमा तक जड़ीभूत किये दे रही है कि वह उकता कर अपने आपको ऐश्वर्य से बचाने के लिए छटपटा रही है।
हम कितने घाटे में हैं—अनुमान तो करें—
प्रोफेसर हावेर्ड डिंगले जो लन्दन विश्व-विद्यालय के एक प्रख्यात खगोल पिंडों के भौतिकीय एवं रासायनिक विज्ञान के ज्ञाता (एस्ट्रोफिजिस्ट) तथा दर्शन शास्त्र एवं विज्ञान के इतिहास के भी ज्ञाता थे—उनका कथन है कि जब हम उस विज्ञान की प्रकृति के बारे में विचारते हैं, जो आजकल प्रचलित है एवं जिसका उपयोग आजकल हो रहा है, हम ऐसी परिस्थितियां पायेंगे, जिनसे भगवान के दूत भी रोने लगें। यह ऐसा युग नहीं कि आंख मींच कर विज्ञान की शक्ति को महत्व दिया जाय। विज्ञान की सत्यता का ही ध्यान दिया जाय और आध्यात्मिक सत्यों को पूर्ण रूपेण भुला दिया जया तो उसके वही परिणाम हो सकते हैं, जो आज अमेरिका, इंग्लैंड में दिखाई दे रहे हैं। जो सुखद नहीं हैं। अमेरिका का आकाश कभी अवकाश नहीं पाता। वहां हर क्षण कम से कम एक हजार जहाज आकाश में केवल पहरेदारी के लिये गड़गड़ाते घूमा करते हैं। पहरेदारी की चिन्ता भयग्रस्तों को होती है। अमेरिका जैसा भयभीत कोई दूसरा देश नहीं, यह विज्ञान की देन है।
हवाई जहाजों के अतिरिक्त वहां हजारों कारखाने, मोटरें, मशीनें चौबीस घण्टे चलते रहते हैं, उससे वातावरण में गन्दी गैसें छाई रहती हैं, शोर इतना होता है कि एक शहर में जितना शोर होता है, यदि उसे विद्युत शक्ति में बदल दिया जाय तो सारे शहर के उपभोग की आवश्यकता को पूरा करके भी बहुत-सी विद्युत शेष बच जायेगी। गन्दी गैसों के कारण वहां नई-नई तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जो केवल अमेरिका में ही पाई जाती हैं, उनके उपचार के लिये उसे निरन्तर नई-नई औषधियों की खोज में लगे रहना पड़ता है। तीन चौथाई विज्ञान वहां एक चौथाई विज्ञान के दुष्परिणामों की रोकथाम भर के लिये है, होता उल्टा है, विज्ञान जितना बढ़ता है, वहां की समस्यायें उतनी ही जटिल होती जा रही हैं। वहां के मूर्धन्य मनीषी आइन्स्टीन तक को इसीलिये कहना पड़ा था—‘‘विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म की प्रगति न हुई तो संसार अपनी इस भूल के भयंकर दुष्परिणाम आप ही भुगतेगा।’’
चौबीस घण्टे शोर के कारण वहां 70 प्रतिशत लोगों के मस्तिष्क खराब हैं। आत्म-हत्यायें और हत्यायें सबसे अधिक अमेरिका में होती हैं, 70 प्रतिशत अमेरिकन नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, अन्यथा उनके मस्तिष्क इतने अशान्त हैं कि उन्हें स्वाभाविक नींद लेना भी कठिन हो जाता है। दाम्पत्य-जीवन जितना अमेरिका और इंग्लैंड में क्लेशपूर्ण है, उतना संसार के किसी भी भाग में नहीं। अमेरिका में एक कहावत प्रचलित है, ‘रात को विवाह प्रातः सम्बन्ध-विच्छेद’ (नाइट मैरिजेज मार्निंग डाइवर्स)। इंग्लैंड में कोई स्त्री ‘मैं तलाक देती हूं’ (आई डाइवर्स यू) तीन बार कह दे तो उन्हें कानूनन तलाक की अनुमति मिल जाती है। यह घटनायें बताती हैं कि विज्ञान और यन्त्रीकरण की प्रगति वाले इन देशों का आन्तरिक जीवन कितना खोखला कष्टपूर्ण और विभ्रान्त है।
यह स्थिति ऐश्वर्य सम्पन्न लोगों के लिए ही नहीं है। उन लोगों के लिए भी उसी प्रकार विकराल है जिनकी दौड़ ऐश्वर्य का लक्ष्य सामने रखकर चल रही है। ऐश्वर्यशाली अपने ऐश्वर्य में आत्मा को खोया अनुभव करते हैं तो ऐश्वर्य—अभिलाषी अपनी आकांक्षा के दहर में आत्मा को दग्ध पा रहे हैं।
इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है कि यन्त्र सभ्यता को छोड़कर समाज पीछे चला जाये। यह एक और बड़ी गलती होगी। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने मूल्यों को सुरक्षित रखते हैं यन्त्रों द्वारा श्रम की थकान को कम करें, न कि नष्ट। इसके लिए बदलती आज की मान्यताओं पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने की आवश्यकता है।
प्रकृति ने उतने साधन पहले से ही जुटाकर रखे हैं जिनका यथोचित और उपयोगी मात्रा में उपयोग किया जाता रहे तो हर व्यक्ति सुखी जीवन, नीरोगिता का जीवन, पारस्परिक शान्ति और सद्भाव का जीवन जी सकता है, पर सब इन्द्रियों की सामर्थ्य से बहुत अधिक और असीम उपभोग की तृष्णा बढ़ी तो स्वाभाविक था मनुष्य कोई ऐसा रास्ता अपनाता जिसमें कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकता। इस महत्वाकांक्षा और अनियन्त्रित भोग बुद्धि ने अभियांत्रिकी को जन्म दिया। हाथ का काम, पैर का काम, यहां तक कि बुद्धि का काम भी मशीनों ने ले लिया। हाथ-पांव चलते रहें इसके लिए परमात्मा ने मनुष्य में इच्छायें पैदा कीं, पर उसका यह उद्देश्य कभी नहीं रहा कि इच्छायें उसकी साध्य बन जायें। यही भूल हुई जिससे मनुष्य स्वयं मशीन बनता जा रहा है। हर काम मशीन करे, तो फिर हाथ, पांवों में जंग लगना स्वाभाविक ही है, बीमारियां बढ़नी स्वाभाविक हैं, ‘‘खाली दिमाग शैतान का घर’’ की उक्ति के अनुसार बौद्धिक भ्रष्टाचार, पाप और पतन की सम्भावनाओं का विकास स्वाभाविक ही था सो इन दिनों वही हो भी रहा है। यन्त्रीकरण के दुष्परिणाम भुगत रहे हैं सो अलग आज तो यह साधन ही सामूहिक सर्वनाश के कारण बन बैठे हैं।
पैदल चलना भी आवश्यक
आये दिन वायुयान दुर्घटनाओं रेलों की भिड़न्त और उससे सैकड़ों लोगों की दुर्घटनायें समाचार पत्रों में आती रहती हैं, उन्हें भी आकस्मिक व अपवाद के रूप में ही माना जाता है। आज जब कि संसार की जनसंख्या भीषण रूप से बढ़ रही है सम्भव है इन दुर्घटनाओं का मूल्य न आंका जाता हो, पर यातायात के यान्त्रिक साधनों की वृद्धि ने जन-जीवन को दुर्घटनाओं से कितना भयाक्रान्त कर दिया है इसकी कल्पना भी कम दुःखद नहीं है। यह रोग चूंकि अभी भारतवर्ष में अधिक नहीं फैला इसलिए उधर ध्यान कम जाता है, पर इस दृष्टि से पश्चिमी देशों का निरीक्षण करें तो यही कहना पड़ेगा—मनुष्य यातायात में इतनी शीघ्रता न कर पैदल चलने में ही राजी रहता तो कहीं अधिक नफे में रहता।
अमरीका में रास्तों पर चलने वाले 10 में 17 व्यक्ति मोटर, ठेलों द्वारा कुचल दिये जाते हैं, इंग्लैंड में प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत सड़कों पर चलने वाले लोग घर के बजाय स्वर्ग पहुंचा दिये जाते हैं। इटली में कारों की संख्या कम है 200 में से 9 के पास ही कारें होती हैं तो भी यह कम करें ही 56 प्रतिशत पथिकों को कुचल डालती हैं और जापान जिसका औसत इटली से भी कम है प्रतिवर्ष 100000 यात्रियों में से 402.2 आदमियों को पीस डालता है। इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करने पर पता चला कि संसार में आज यातायात दुर्घटनाओं से उतने लोग मरते हैं जितने संक्रामक बीमारियों से भी नहीं मरते।
पैदल चलने में शरीर की नस-नस हिल अवश्य जाती है, पर उससे शरीर में कितनी शक्ति आती है यह भी किसी से छिपा नहीं। एक मील चलने से शरीर को जो व्यायाम करना पड़ता है उससे मनुष्य को 1 दिन के लिए अतिरिक्त शक्ति मिलती है और 1 दिन की आयु बढ़ जाती है। प्राचीनकाल में लोग लम्बी-लम्बी यात्रायें बहुत थोड़े समय में किया करते थे उनमें इतनी शक्ति और स्फूर्ति बनी रहती थी जब कि आज मोटरों और कारों पर चलने वाले लोग आराम से यात्रायें करने पर भी घर वापिस आने पर हारे, थके, टूटे और बीमार से लगने लगते हैं। प्राचीनकाल में तीर्थयात्राओं और परिक्रमाओं का विधान था, उसमें जहां शुद्ध और सुसंस्कृत वातावरण का लाभ लेने का भाव था वहां हमेशा घरों में बैठे रहने के आलस्य को पैदल यात्राओं द्वारा भगाना भी उद्देश्य था। इन यात्राओं से परिक्रमाओं से लोग भरपूर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते थे।
मोटर हों चाहे रेलें उनका धुआं और गैस यात्रियों के मस्तिष्क पर बुरा असर डालती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डा. रौस.ए. मैकफारलैण्ड का कथन है कि मनुष्य को नियमित रूप से स्वस्थ और ताजा रखने के लिए 18 से 50 फुट प्रति सेकेंड की गति से चलती हुई 1 घन मीटर ताजी हवा की आवश्यकता होती है इसी प्रकार वायु में नमी की 15 प्रतिशत से कमी भी स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर बुरा असर डालती है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सामूहिक अपान और मुंह से निकाली हुई दूषित वायु मोनो ऑक्साइड पैदा करती है जिससे देखने में आराम से यात्रा करने वाले यात्री की आंख, कान, मस्तिष्क और रक्त में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यह विकार जहां यात्रियों के लिए स्वास्थ्य-घातक होते हैं वहां ड्राइवरों के लिए ज्ञान नाशक। उनके मस्तिष्क के तन्तु और मांस-पेशियां नियन्त्रण में रहना छोड़ देती हैं दुर्घटनायें उसी का प्रतिफल होती हैं आज सारा योरोप उसके निश्चित दुष्परिणाम भुगत रहा है।
इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन?
यह कहना चाहिए कि आज योरोप में यात्रा करना उतना ही जोखिम भरा हो गया है जितना कि तूफानी समुद्र में टूटी हुई नाव लेकर चलना। स्वीडन में 1 लाख वाहन प्रतिवर्ष 76.1 आदमियों को रौंद डालते हैं, अमेरिका में अनेक सुरक्षा साधनों के बावजूद 52.6 न्यूजीलैण्ड में, 53.8 तो डेनमार्क के 1 लाख रजिस्टर्ड वाहन 101.8 यात्रियों को मार डालते हैं। फ्रांस उससे भी आगे है वह अपनी इतनी मोटरों, कारों और ठेलों द्वारा 112.9 व्यक्तियों को पीस डालता है तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की गाड़ियां क्रमशः 153 और 159.8 व्यक्तियों को जिन्दा चबा जाती हैं। यह अकाल मृत आत्मायें, आकाश और वातावरण में हा-हाकार करती घूमती होंगी तो उससे मनुष्य जाति का सूक्ष्म अन्तःकरण कितना अशान्त होता होगा उसकी कल्पना करना भी कठिन है।
सारा संसार घण्टे भर की यात्रा की सीमा में आ जाय उससे लाभ कुछ नहीं हानियां अपार हैं। इसलिए यातायात के साधनों में वृद्धि द्वारा सारे संसार को एक बिन्दु पर ला देने का तर्क कोरी मूर्खता है। जब यह साधन नहीं थे इतिहास बताता है कि तब भी सारा संसार इतने ही समीप था। समीपता विचारों, सिद्धान्तों और मानवीय आदर्शों की ही अच्छी हो सकती है, उसके दूसरे माध्यम हैं गन्दगी बढ़ाने वाले शरीरों की समीपता से जो विकास बढ़ने चाहिये आज संसार में वही बढ़ रहे हैं। अतएव इन साधनों के विकास के प्रयत्नों का अच्छा कदापि नहीं कहा जा सकता।
आज सब कुछ इससे उल्टा हो रहा है। योरोप में प्रतिवर्ष 5000 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं और लगभग 1 लाख दुर्घटनाओं के शिकार होकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं फिर भी प्रयत्न यह हो रहे हैं कि यहां अभी 200 व्यक्तियों पर 25 मोटरों का औसत है वहां जल्दी ही 200 व्यक्तियों पर 50 और 75 का औसत हो जाये। यदि विकास की गति इसी तरह बढ़ती गई तो एक दिन वह भी आ सकता है जब न तो पैदल चलने के लिए पगडंडियां रह जायेंगी और न ही पैदल यात्री। तब लोग अपने आप ही दुर्घटनाओं के शिकार होकर मर जाया करेंगे। आखिर यातायात के यह कृत्रिम साधन बढ़ेंगे तो दुर्घटनायें और मृत्यु दरें भी 79 व 37 प्रतिशत से शत प्रतिशत होंगी ही। तब साहित्य भी पैदल चलने के लाभों के स्थान पर यातायात की दुर्घटनाओं का ही लिखा जाया करेगा जो इन पंक्तियों से भयंकर ही होगा। उस विभीषिका से बचाव अभी हो सकता है।
भौतिक प्रगति आत्मिक अवनति
यह बात केवल यातायात तक ही सीमित नहीं। आज के नागरिक की दिनचर्या, रहन-सहन और आदतें देखकर उसकी जो तस्वीर बनती है वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य का जीवन भी एक यन्त्र की तरह हो गया है। पाषाण, लौह और ताम्रयुगीन विभाजनों के साथ वर्तमान सन्दर्भों को देखा जाय तो इसे निश्चित ही यन्त्र युग कहना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन और यान्त्रिक उपकरण परस्पर इतने घनिष्ठ हो गये हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से विलग कर पाना ही असम्भव है। उस क्षण की स्थिति को कल्पनांकित ही नहीं किया जा सकता, जब कि मनुष्य का जीवन यन्त्रों की सुविधा से एकदम रहित हो जाय। मिल कपड़े बनाते हैं, कारखानों में खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, साबुन, तेल, ईंधन आदि सब किसी न किसी रूप में मशीनों से सम्बद्ध मिलेंगे। यहां तक कि जिस रोशनी का हम रात दिन उपयोग करते हैं वह भी रात दिन मशीनों द्वारा ही पैदा होती है और हम तक पहुंचाई जाती है।
हम जिन परिस्थितियों, वातावरणों तथा वस्तुओं के संसर्ग में रहते हैं, उनका हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारा उन पर। मनुष्य से समाज बनता है और समाज मनुष्य को बनाता है। मनुष्य अपने आस-पास के वातावरण से प्रभावित होता है और वातावरण मनुष्य से प्रभावित होता है। प्रभाव पड़ने या पैदा होने की यह प्रक्रिया दोनों ओर से होती है एकांगी कभी नहीं। लेकिन यन्त्रों के सम्बन्ध में कुछ ओर ही सचाई है। सिलाई की मशीन पांव चलाने से चलती है और पांव रोक देने पर बन्द हो जाती है। बाद में वह कोई गति नहीं करती, परन्तु दिन-रात सिलाई मशीन पर बैठने वालों के पांव कभी-कभी अपने आप भी चलने लगते हैं। यह आदतन प्रभाव है।
आदतन प्रभाव की तरह ही मनुष्य भावनाओं से भी प्रभावित होता है और आजकल ‘यान्त्रिक-सभ्यता’ की समीक्षा करते समय इसी भावनात्मक प्रभाव की चर्चा की जाती है। हालांकि संसर्ग के अतिरिक्त इसके और भी कई कारण हैं। इसी तथ्य की ओर इशारा करते हुए प्रसिद्ध विचारक नीत्शे ने कहा था—‘‘यन्त्र जितनी तीव्रता से प्रगति कर रहा है उसी अनुपात से मनुष्य की धर्म सम्वेदना का ह्रास हो रहा है। समस्त भौतिक सुविधाओं से सम्पन्न हो जाने पर भी मनुष्य इतना आत्म-विपन्न हो रहा है कि बीसवीं शती के अन्त तक वह एकदम खोखला हो जायेगा और भयंकर रूप से दुःखी रहने लगेगा।’’
इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक आधुनिक विचारक का कथन है कि—‘‘आज के युग में जीने वाले व्यक्ति की स्थिति विचित्र कम और शोचनीय अधिक है। समस्त मानवीय सम्बन्ध अब केवल वित्तीय स्तर पर बनते हैं अन्य सभी माध्यमों को या तो नगण्य घोषित कर दिया गया है अथवा फिर यान्त्रिकता से जकड़े हुए नये समाज में वे किसी अज्ञात प्रक्रिया द्वारा स्वतः डूबते जाते हैं।’’ चूंकि मनुष्य समाज का एक अंग है और इस नाते उसे दूसरे अन्य अंगों के सम्पर्क में आना पड़ता है। मानवता का तकाजा तो यह है कि हम अपने पड़ौसियों के दुःख-सुख में काम आयें, उनकी खैर-खबर रखें और कुशलक्षेम से अवगत रहने के साथ-साथ समय-समय पर काम भी आयें। परन्तु पड़ौसियों के प्रति यह आत्मीयता का भाव धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानगरों की स्थिति तो यह है कि वहां रहने वाला एक व्यक्ति अपने पड़ौसी के दुःख दर्द में साथ देने के स्थान पर उसे जानता तक भी नहीं शहरों और कस्बों के नागरिकों को भी अपनी समस्याओं से कम ही फुरसत मिल पाती है और इस फुरसत को पड़ौसियों से मेल-जोल बनाने के स्थान पर सिनेमा देखने या सैर करने में गुजारना अधिक अच्छा समझते हैं।
पड़ौसियों से कटे रहने तक की ही बात सीमित रहती तो इतनी शोचनीय स्थिति नहीं आती। आश्चर्य तो तब होता है जब लोगों को अपने रिश्तेदारों और सम्बन्धियों से सम्पर्क रखने का भी समय नहीं मिलता। यही नहीं आदमी अपने बीमार पत्नी के पास बैठने की अपेक्षा दिन भर की थकान उतारने के लिए रेडियो सुनना और घूमने निकल जाना अधिक अच्छा समझता है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई में क्या स्थिति है—इससे अनभिज्ञ रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने शहर में रहने वाले मित्रों और सम्बन्धियों के घर न जाये ही महीनों बीत चुके हैं। अर्थात् मनुष्य समाज में रहता तो है अवश्य, पर समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं—या तो वह अनभिज्ञ है अथवा जान-बूझकर उनकी उपेक्षा करता है।
इतना एकाकीपन होने के बावजूद भी मनुष्य आर्थिक दृष्टि से किसी से सम्पर्क सूत्र कायम करने में चूकना नहीं चाहता। कारण कि यन्त्रों की बाढ़ ने मनुष्य का श्रम हल्का किया है और उसकी सुविधाएं बढ़ाई हैं। इसलिए उपभोग सामग्रियों से बाजार भरे हैं। जो समर्थ हैं, वे उन्हें खरीद सकते हैं तथा उनका उपभोग कर सकते हैं। इस कारण असमर्थ और विपन्न व्यक्तियों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट होता है तथा वे भी उनका वैसा ही उपयोग करने के लिए ललक उठते हैं। बेशक उन्हें खरीदने के लिए अतिरिक्त आर्थिक साधन चाहिए। इस समर्थता और असमर्थता ने सम्पन्नता को ही प्रतिष्ठा का बिन्दु बना दिया है। जिसे हर कोई बींधना चाहता है और उसे बींधने में इस कदर लवलीन है कि उसे अपने आस-पास की चीजें भी नहीं दिखाई देतीं।
यान्त्रिक संसर्ग का जहां तक प्रश्न है मशीनी वातावरण में रहने का अपना एक अलग प्रभाव है। लेकिन उससे भी अधिक बुरी तरह प्रभावित और आत्म-विपन्न कर देने वाली स्थिति, बदलते दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई है। जिसने वित्तीय—दशा को ही सर्व प्रधान बना दिया और उसे पूरा करने के लिए मनुष्य इतना मदमत्त होकर दौड़ने लगा कि एकाकीपन, संत्रास, आत्म-विपन्नता, स्वकेन्द्रित मनोवृत्तियां, कुण्ठाएं और विक्षेप उसे चारों ओर से छेदने लगे हैं। मशीनों के संसर्ग का एक व्यवस्थित कार्य-क्रम है, जो सुखी जीवन की एक निश्चित गारंटी है। परन्तु उसके बावजूद और-और कारण जो यान्त्रिक सभ्यता को दोषों से विषाक्त करते हैं मनुष्य को तनावग्रस्त तथा असुरक्षित बनाते हैं।
अब से 25-50 साल पहले युवकों के सामने जीवन में प्रवेश करने का यह एक रेडीमेड तरीका था कि पढ़ना-लिखना और डिग्री प्राप्त करना तथा उसके बाद नौकरी से लग जाना या शिक्षा प्राप्त करना। नौकरी धन्धे से लगने और परिवार बस जाने के बाद भी युवक को परिवार का आर्थिक संरक्षण मिलता रहता था। इसका एक कारण तो यह था कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी। जिसमें सभी सदस्यों के हित परस्पर जुड़े हुए थे तथा प्रत्येक एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों का अनुभव करते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और एकाकी परिवार अधूरी-अधकचरी स्थिति में जीते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आशा बांधे रहते हैं। अपने माता-पिता और सहोदर भाई-बहिनों से सिकुड़ कर मानवी गतिविधियों का केन्द्र पत्नी, बच्चे और स्वयं तक ही सीमित हो गया है। जो संयुक्त परिवार किसी प्रकार टूटने से बचे हुए हैं, जिनके सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कुछ दायित्व अनुभव करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सजग रहते हैं, वे भी नौकरी और रोजगार करने के लिए बिखरे पड़े हैं। कहने का अर्थ यह कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने के चक्कर में हम और अधिक दीन-हीन व एकाकी बनते जा रहे है। यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग अपने माता-पिता और सहोदर भाई-बहिनों के लिए ही कुछ करना व्यर्थ समझते हों वे पड़ौसियों और मित्रों के लिए कुछ करने की क्या सोचेंगे?
अकेलेपन का यह मानसिक प्रभाव नगरीय लोगों में अधिकांशतः है। इसकी तुलना सौ वर्ष पुराने समाज से करते हुए लिखा गया है—‘‘उन्नीसवीं सदी का मनुष्य अपनी आत्म सम्पन्नता के बल पर ही अनेक दुःख झेलकर भी मानवीयता से भ्रष्ट नहीं हो पाता था और उसकी इस आत्म-सम्पन्नता के पीछे संयुक्त परिवार प्रथा, धर्म और संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ था। जब कि बीसवीं सदी का मनुष्य इतना बर्हिप्रविष्ट हो गया है कि सामान्यतया स्वयं को नगण्य व एकाकी मानता हुआ किसी भी क्षण अपने आपको दूसरों के हाथों में छोड़ देने के लिए विवश हो जाता है या मजबूरन अपने को तैयार करता है।’’
यान्त्रिक सभ्यता में मनुष्य की दृष्टि का केन्द्र बिन्दु बदला है और उसने मानवीयता के स्थान पर आर्थिकता को व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा माना है। वही उसका अपना जीवन भी एकरस और उसके कारण विद्रोही बना है। हाल ही में पिछले वर्षों ब्राक्स में एक अद्भुत घटना घटी। एक बस ड्राइवर अपनी बस समेत अनायास लापता हो गया। तीन-चार दिन बाद वह बस समेत फ्लोरिडा में पकड़ा गया। इस बीच अखबारों में वह बड़ी चर्चा का विषय बन गया। बस कम्पनी के मालिकों ने जब उससे भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछले सात वर्षों से वह एक ही रूट पर बस चलाते-चलाते और उन्हीं स्थानों पर बार-बार बस रोकते-रोकते बुरी तरह बोर हो गया है। परिवर्तन के लिए ही उसे पलोरिडा आने का निर्णय लेना पड़ा।
जैसा कि कहा जा चुका है कि मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा आज अधिक सुनिश्चित और व्यवस्थित कार्य-क्रम है। परन्तु उसकी उबाऊ एकरसता ने मनुष्य की चेतना को एकरस बना दिया है और वह इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये एकदम से तैयार नहीं है। इस उबाऊ एकरसता के कारण वह बोरियत अनुभव करता है और उसे तोड़ देने के लिए स्वच्छन्दता, उन्मुक्तता और हिप्पीवाद की अनेकानेक भ्रान्त धाराओं में वह निकलता चाहता है। यन्त्र जिस प्रकार एक ही गति और लय में चलता है उसी प्रकार मनुष्य भी एक ही स्थिति को बार-बार भोगने के लिये अपने आपको विवश अनुभव करता है। कहने का अर्थ यह है कि वह अपने आपको कोल्हू के बैल वाली स्थिति में पाता है, जिसे उसकी प्रवाहमान गतिशील चेतना किसी भी दशा में भोगने को तैयार नहीं है। एक अर्थ शास्त्री के शब्दों में मनुष्य की चेतना ह्रासमान उपयोगिता की भांति सम्वेदना शून्य बनती जा रही है। वह व्यक्ति को इस सीमा तक जड़ीभूत किये दे रही है कि वह उकता कर अपने आपको ऐश्वर्य से बचाने के लिए छटपटा रही है।
हम कितने घाटे में हैं—अनुमान तो करें—
प्रोफेसर हावेर्ड डिंगले जो लन्दन विश्व-विद्यालय के एक प्रख्यात खगोल पिंडों के भौतिकीय एवं रासायनिक विज्ञान के ज्ञाता (एस्ट्रोफिजिस्ट) तथा दर्शन शास्त्र एवं विज्ञान के इतिहास के भी ज्ञाता थे—उनका कथन है कि जब हम उस विज्ञान की प्रकृति के बारे में विचारते हैं, जो आजकल प्रचलित है एवं जिसका उपयोग आजकल हो रहा है, हम ऐसी परिस्थितियां पायेंगे, जिनसे भगवान के दूत भी रोने लगें। यह ऐसा युग नहीं कि आंख मींच कर विज्ञान की शक्ति को महत्व दिया जाय। विज्ञान की सत्यता का ही ध्यान दिया जाय और आध्यात्मिक सत्यों को पूर्ण रूपेण भुला दिया जया तो उसके वही परिणाम हो सकते हैं, जो आज अमेरिका, इंग्लैंड में दिखाई दे रहे हैं। जो सुखद नहीं हैं। अमेरिका का आकाश कभी अवकाश नहीं पाता। वहां हर क्षण कम से कम एक हजार जहाज आकाश में केवल पहरेदारी के लिये गड़गड़ाते घूमा करते हैं। पहरेदारी की चिन्ता भयग्रस्तों को होती है। अमेरिका जैसा भयभीत कोई दूसरा देश नहीं, यह विज्ञान की देन है।
हवाई जहाजों के अतिरिक्त वहां हजारों कारखाने, मोटरें, मशीनें चौबीस घण्टे चलते रहते हैं, उससे वातावरण में गन्दी गैसें छाई रहती हैं, शोर इतना होता है कि एक शहर में जितना शोर होता है, यदि उसे विद्युत शक्ति में बदल दिया जाय तो सारे शहर के उपभोग की आवश्यकता को पूरा करके भी बहुत-सी विद्युत शेष बच जायेगी। गन्दी गैसों के कारण वहां नई-नई तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जो केवल अमेरिका में ही पाई जाती हैं, उनके उपचार के लिये उसे निरन्तर नई-नई औषधियों की खोज में लगे रहना पड़ता है। तीन चौथाई विज्ञान वहां एक चौथाई विज्ञान के दुष्परिणामों की रोकथाम भर के लिये है, होता उल्टा है, विज्ञान जितना बढ़ता है, वहां की समस्यायें उतनी ही जटिल होती जा रही हैं। वहां के मूर्धन्य मनीषी आइन्स्टीन तक को इसीलिये कहना पड़ा था—‘‘विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म की प्रगति न हुई तो संसार अपनी इस भूल के भयंकर दुष्परिणाम आप ही भुगतेगा।’’
चौबीस घण्टे शोर के कारण वहां 70 प्रतिशत लोगों के मस्तिष्क खराब हैं। आत्म-हत्यायें और हत्यायें सबसे अधिक अमेरिका में होती हैं, 70 प्रतिशत अमेरिकन नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, अन्यथा उनके मस्तिष्क इतने अशान्त हैं कि उन्हें स्वाभाविक नींद लेना भी कठिन हो जाता है। दाम्पत्य-जीवन जितना अमेरिका और इंग्लैंड में क्लेशपूर्ण है, उतना संसार के किसी भी भाग में नहीं। अमेरिका में एक कहावत प्रचलित है, ‘रात को विवाह प्रातः सम्बन्ध-विच्छेद’ (नाइट मैरिजेज मार्निंग डाइवर्स)। इंग्लैंड में कोई स्त्री ‘मैं तलाक देती हूं’ (आई डाइवर्स यू) तीन बार कह दे तो उन्हें कानूनन तलाक की अनुमति मिल जाती है। यह घटनायें बताती हैं कि विज्ञान और यन्त्रीकरण की प्रगति वाले इन देशों का आन्तरिक जीवन कितना खोखला कष्टपूर्ण और विभ्रान्त है।
यह स्थिति ऐश्वर्य सम्पन्न लोगों के लिए ही नहीं है। उन लोगों के लिए भी उसी प्रकार विकराल है जिनकी दौड़ ऐश्वर्य का लक्ष्य सामने रखकर चल रही है। ऐश्वर्यशाली अपने ऐश्वर्य में आत्मा को खोया अनुभव करते हैं तो ऐश्वर्य—अभिलाषी अपनी आकांक्षा के दहर में आत्मा को दग्ध पा रहे हैं।
इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है कि यन्त्र सभ्यता को छोड़कर समाज पीछे चला जाये। यह एक और बड़ी गलती होगी। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने मूल्यों को सुरक्षित रखते हैं यन्त्रों द्वारा श्रम की थकान को कम करें, न कि नष्ट। इसके लिए बदलती आज की मान्यताओं पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने की आवश्यकता है।