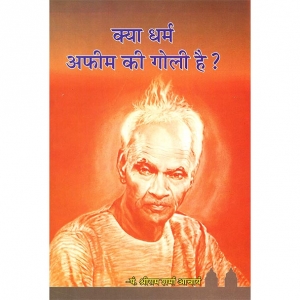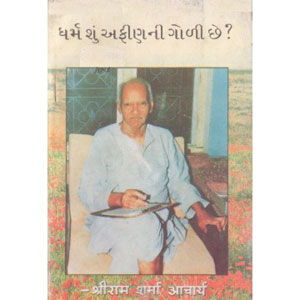क्या धर्म अफ़ीम की गोली है 
सांस्कृतिक एकता का आधार—धर्म
Read Scan Version
सभ्यता और संस्कृति इस युग के दो बहु-परिचर्चित विषय हैं। आस्थाओं और मान्यताओं को संस्कृति और तदनुरूप व्यवहार, आचरण को सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। दुनिया में जितनी जातियां हैं उतनी सभ्यतायें और संस्कृतियां भी हैं किन्तु यदि भारतीय दर्शन को निरीक्षक मानकर विश्लेषण करें तो पता चलता है कि सभ्यता और संस्कृतियां अनेक नहीं हो सकतीं। मानवीय सभ्यता या संस्कृति कहें या चाहे जो भी नाम दें मानवीय दर्शन सर्वत्र एक ही हो सकता है, मानवीय संस्कृति केवल एक हो सकती है दो नहीं क्यों कि विज्ञान कुछ भी हो मानवीय प्रादुर्भाव का केन्द्र बिन्दु और आधार एक ही हो सकता है। इनका निर्धारण जीवन के बाह्य स्वरूप भर से नहीं किया जा सकता। संस्कृति को यथार्थ स्वरूप प्रदान करने के लिए अन्ततः धर्म और दर्शन की ही शरण जाना पड़ेगा।
संस्कृति का अर्थ है मनुष्य का भीतरी विकास। उसका परिचय व्यक्ति के निजी चरित्र और दूसरों के साथ किये जाने वाले सद्व्यवहार से मिलता है। दूसरों को ठीक तरह समझ सकने और अपनी स्थिति एवं समझ धैर्यपूर्वक दूसरों को समझा सकने की स्थिति भी उस योग्यता में सम्मिलित कर सकते हैं। जो संस्कृति की देन है।
आदान-प्रदान एक तथ्य है जिसके सहारे मानवी प्रगति के चरण आगे बढ़ते-बढ़ते वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। कृषि, पशु पालन शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, विज्ञान, दर्शन जैसे जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के सम्बन्धित प्रसंग किसी एक क्षेत्र या वर्ग की वपौती नहीं है। एक वर्ग की उपलब्धियों से दूसरे क्षेत्र के लोग परिचित हुए हैं। परस्पर आदान-प्रदान चले हैं और भौतिक क्षेत्र में सुविधा सम्वर्धन का पथ-प्रशस्त हुआ है। ठीक यही बात धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध में भी है। एक ने अपने सम्पर्क क्षेत्र को प्रभावित किया है। एक लहर ने दूसरी को आगे धकेला है। लेन-देन का सिलसिला सर्वत्र चलता रहा है। मिलजुल कर ही मनुष्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इस समन्वय से धर्म और संस्कृति भी अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित किया है।
अब दुनिया में कोई नस्ल ऐसी नहीं बची जो पूरी तरह रक्त शुद्धि का दावा कर सके। जातियों के बीच प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बेटी व्यवहार चलते रहे हैं और नस्लों के मूल रूप में आश्चर्य जनक परिवर्तन हो गया है। भारत वंशी लोगों के रक्त में आर्य और द्रविड़ रक्त का सम्मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि दोनों से मिलकर एक तीसरी अथवा संयुक्त जाति बन गई है। इसी प्रकार एक सभ्यता पर दूसरी सभ्यता के निकट आने का भारी प्रभाव पड़ा है। भारत में पिछले एक हजार वर्ष में मुस्लिम और ईसाई सभ्यताएं आती रही हैं। उनके पूर्ण अनुयायी कितने बने यह बात पृथक है। सामान्य जनमानस ने उनका बहुत कुछ प्रभाव ग्रहण किया है। प्रचलित भारतीय पोशाक ऐसी नहीं है। जिसे दो हजार वर्ष पुरानी कहा जा सके। इसी प्रकार रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं में भी अनजाने ऐसे तत्व का समावेश होता रहा है जिसे खुले मन से न सही हिचकिचाहट के साथ—समन्वय स्वीकार किया जा सके।
यह सभ्यताओं का समन्वय एवं आदान-प्रदान उचित भी है और आवश्यक भी। कट्टरता के कटघरे में मानवी विवेक को कैद रखे रहना असम्भव है। विवेक दृष्टि जागृत होते ही इन कटघरों की दीवारें टूटती हैं और जो रुचिकर या उपयोगी लगता है उसका बिना किसी प्रचार या दबाव के आदान-प्रदान चल पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए कट्टरपंथी प्रयास सदा से हाथ-पैर पीटते रहे हैं, पर यह कठिन ही रहा है। हवा उन्मुक्त आकाश में बहती है। सर्दी-गर्मी का विस्तार व्यापक क्षेत्र में होता है। इन्हें बन्धनों में बांधकर कैदियों की तरह अपने ही घर में रुके रहने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। सम्प्रदाओं और सभ्यताओं में भी यह आदान-प्रदान अपने ढंग से चुपके चुपके चलता रहा है। भविष्य में इसकी गति और भी तीव्र होगी।
धर्म और संस्कृति के बारे में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। वे दोनों ही सार्वभौम हैं उन्हें सर्वजनीन कहा जा सकता है। मनुष्यता के टुकड़े नहीं हो सके। सज्जनता की परिभाषा में बहुत मतभेद नहीं है। शारीरिक संरचना की तरह मानवी अन्तःकरण की मूल सत्ता भी एक ही प्रकार की है भौतिक प्रवृत्तियां भी लगभग एक-सी हैं। एकता व्यापक है और शाश्वत। पृथकता सामयिक है और क्षणिक। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। एक ही धरती पर पैदा हुए हैं। एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। एक ही सूर्य से गर्मी पाते हैं और बादलों के अनुदार से एक ही तरह अपना गुजारा करते हैं फिर कृत्रिम विभेद से बहुत दिनों तक बहुत दूरी तक किस प्रकार बंधे रह सकते हैं। औचित्य को आधार मानकर परस्पर आदान-प्रदान का द्वार जितना खोलकर रखा जायगा उतना ही स्वच्छ हवा और रोशनी का लाभ मिलेगा। खिड़कियां बन्द रखकर हम अपनी विशेषताओं को न तो सुरक्षित रख सकते हैं और न स्वच्छ हवा और खुल धूप से मिलने वाले लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। संकीर्णता अपना कर पाया कम, और खोया अधिक जाता है। एकता की दिशा में हम आगे बढ़ें तो इसमें पूर्वजों के प्रति अनास्था नहीं वरन् श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति है। पूर्वज अपने पूर्वजों की विरासत को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए भी अपने बुद्धिबल और बाहुबल से नये अनुभव एकत्रित करते, लाभ कमाते और साधन जुटाते रहे हैं। इसमें पूर्वजों को सन्तोष ही हो सकता है। साथ ही गर्व भी। अपनी संतान पर कोई अभिभावक यह बन्धन नहीं लगाता कि हममें अधिक शिक्षा या सम्पत्ति सन्तान को नहीं कमानी चाहिए। हममें अधिक यश या कौशल अर्जित नहीं करना चाहिए। बन्धन लगाना तो दूर—समझदार अभिभावक अपने से अधिक प्रगति करने के लिए अपने उत्तराधिकारियों को उत्साहित और उत्तेजित करते हैं। ऐसी दशा में पूर्वजों की तुलना में एकता के क्षेत्र में हम कुछ कदम और आगे बढ़ सके तो इसमें असमंजस की कोई बात नहीं है। इसमें पूर्वजों की अवज्ञा जैसी कोई प्रश्न उठता नहीं नहीं। पिताजी यदि 60 वर्ष जियें और बेटा 70 वर्ष जी सके तो इसमें दुःख मानने की कोई बात नहीं है। सदाशयता, शालीनता, एकता और विवेकशीलता की दिशा में प्रगति करना मानवी प्रगति के इतिहास में एक अच्छी कड़ी और जोड़ देना ही कहा जा सकता है।
अब राष्ट्रवाद के दिन लदते जा रहे हैं। देशभक्ति के जोश को अब उतना नहीं उभारा जाता जिसमें अपने ही क्षेत्र या वर्ग को सर्वोच्च ठहराया जाय अथवा विश्व विजय करके सर्वत्र अपना ही झण्डा फहराने का उन्माद उठ खड़ा हो। ऐसी पक्षपाती और आवेशग्रसित देशभक्ति अब विचारशील वर्ग में नापसन्द की जाती है और विश्व नागरिकता की वसुधैव कुटुम्बकम् की बात को महत्व दिया जाता है। विश्व एकता के सिद्धान्त को मान्यता मिली है और राष्ट्र संघ बना है। इस दिशा में प्रगति के चरण धीमे उठ रहे हैं, यह चिन्ता का प्रसंग है। अपेक्षा यही की जाती है कि संसार की व्यापक समस्याओं का समाधान विश्व एकता के बिना और किसी प्रकार सम्भव न हो सकेगा। एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति अपना कर ही उज्ज्वल भविष्य की, विश्व शान्ति की स्थापना हो सकती है। यह तथ्य मानवी विवेक ने स्वीकार कर लिया है और विभेद उभारने वाले तत्वों को अमान्य ठहराया जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी ऐसी ही व्यापक एकता उत्पन्न करने के लिए वातावरण बनाना होगा। राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद की तरह सभ्यतावाद की कट्टरता को भी अगले दिनों क्रमशः अधिक शिथिल करते चलने की आवश्यकता पड़ेगी। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए ऐसे एकतावादी विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है जिसमें अपने ही पक्ष को सर्वोपरि ठहराये जाने का आग्रह न हो। अपने पराये का भेदभाव न करके औचित्य, न्याय तथ्य और विवेक को ही जब मान्यता दी जायगी तो फिर उपयोगिता स्वीकार करने की मनःस्थिति बन जायगी तब जहां से भी—जितनी मात्रा में तथ्य दृष्टिगोचर होगा स्वीकार किया जायगा। इसके लिए किसी को खेद मनाने की आवश्यकता न होगी कि हमारी अमुक मान्यताओं को सर्वाश में जागृत विवेक ने स्वीकार नहीं किया। पिछला पैर उठाकर ही अगला पैर आगे रखा जाता है। लम्बी मंजिल इसी प्रकार पूरी होती है। आगे बढ़ना है तो पीछे का पैर अपने स्थान पर जमाये रहने का अग्रह नहीं चल सकता।
अंग्रेजी में संस्कृति का अर्थ बोधक शब्द है ‘कलचर’ इसका तात्पर्य है—सभ्यता। रहन-सहन एवं सोचने विचारने का तरीका। अपने नाम, रूप, धन, परिवार, क्षेत्र, भाषा, धर्म आदि की तरह ही अपने रहन-सहन की पद्धति भी लोगों को प्रिय लगती है। यह प्रियता बहुधा पक्षपात के रूप में बदल जाती है। जो अपने को श्रेष्ठ दूसरों को निकृष्ट मानने की तरह है। अपने परिकर एवं सरंजाम के सम्बन्ध में भी वैसी ही मान्यता बन जाती है। इसमें पूर्वाग्रह और पक्षपात का गहरा पुट रहता है। यद्यपि वह लगता ऐसा है मानो सत्य अपने ही हिस्से में आया है। और दूसरे सभी गलत सोचते और झूठ बोलते हैं। अन्यान्य मतभेदों की तरह संस्कृति सम्बन्धी मतभेद भी एक है जिसके लिए बहुत बार भयंकर युद्ध होते रहे। व्यक्तिगत जीवन में भी विद्वेष, घृणा, आक्रमण, प्रतिरक्षा जैसी विडम्बनाएं अनेक बार संस्कृति के नाम पर भी खड़ी होती रही हैं। और उनसे मनुष्य जाति को धन, जन, नीति, सद्भावना, शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से भारी हानि उठानी पड़ी है। इस प्रकार जहां संस्कृति का मूल अस्तित्व व्यक्ति और समाज के कल्याणकारी तत्व पर आधारित है वहां उसके प्रति अत्युत्साह और दुराग्रह में विद्वेष के विष बीज भी कम मात्रा में भरे हुए नहीं हैं। योरोप में ईसाई धर्म के प्रति और एशिया में इस्लाम धर्म के प्रति अत्युत्साह ने जिस निष्ठुरता का परिचय दिया है, उससे उन संस्कृति प्रेमियों का गौरव बढ़ा नहीं। उन धर्मों की गरिमा अन्तःकरण की गहराई में प्रवेश न कर सकी यद्यपि बहुतों ने भयभीत होकर अथवा लोभ लाभ की दृष्टि से उन्हें स्वीकार अवश्य कर लिया।
संस्कृति शब्द को सभ्यता से पृथक रखा जा सके तो अर्थ का अनर्थ होने से बच सकता है। धर्म और सम्प्रदाय के सम्बन्ध में भी यही बात होनी चाहिए। धर्म एक चीज है और सम्प्रदाय दूसरी। सम्प्रदायवाद-धर्म तत्व का समर्थक ही हों यह आवश्यक नहीं। बहुत-सी रिवाजें एवं मान्यताएं ऐसी हो सकती हैं जो प्राचीन होने के साथ-साथ लोक प्रिय बन गई हों और अनेकों व्यक्ति उसके समर्थक अनुयायी हों, इतने पर भी उनका बहुत-सा पक्ष, धर्म भावना के मूल सिद्धान्तों से मेल न खाता हो। भारतीय समाज को ही लें। जाति-पांति के नाम पर ऊंच-नीच की भावना और नर-नारी की असमानता की मान्यता गहराई तक लोगों के मनों में उतर गई है। नीति और न्याय की दृष्टि से उसका तनिक भी औचित्य नहीं है। फिर भी परम्परागत अभ्यास के कारण उसकी जड़ें इतनी नीची चली गई हैं की काटे नहीं कटती। इसी प्रकार हिन्दू धर्म में अथवा अन्य धर्मों में ऐसे ही प्रचलन हो सकते हैं। देवताओं के सामने पशु बलि चढ़ाया जाना, धर्म की मूल मान्यताओं से, उच्चस्तरीय आदर्शों से मेल नहीं खाता फिर भी उसे अनेक धर्मों में मान्यता प्राप्त है।
जिस प्रकार सम्प्रदाय को धर्म का कलेवर भर कह सकते हैं वैसे ही सभ्यताओं में संस्कृति के कुछ तत्व झांकते हुए देखे जा सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, वेश-विन्यास देख कर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती हैं फिर भी उस आवरण को पूरा व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। धर्म एक तत्वज्ञान है जिसमें उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श कर्तृत्व की दिशा में मनुष्य को अग्रगामी बनाने के लिए कुछ नीति-नियमों का निर्धारण है। सम्प्रदाय उस दृष्टिकोण को मानने वाले समुदाय के रहन-सहन का तरीका है। यह तरीका मात्र आदर्शों से ही प्रेरित नहीं होता वरन् परिस्थितियों, साधनों एवं परम्पराओं पर आधारित होता है। उसमें तत्व के सिद्धान्त भी किसी मात्रा में घुले-मिले हो सकते हैं, पर कोई समूचा सम्प्रदाय समूचे धर्म तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उसमें दूसरी चीजों का भी समावेश हो सकता है। किसी सम्प्रदाय का कट्टर अनुयायी सच्चे अर्थों में धर्मात्मा भी होगा यह नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार अनेकानेक सभ्यताओं में भी मानवी संस्कृति की झलक मिल सकती है पर कोई सभ्यता पूरी तरह सुसंस्कृत होने का दावा नहीं कर सकती। यदि ऐसा ही होता तो फिर पृथकता से लेकर विरोध तक के ऐसे तत्व कहीं दिखाई न पड़ते जिनसे टकराव की स्थिति पैदा होती हो।
संस्कृति देश और जाति में विभाजित नहीं हो सकती। वह मानवी है और सार्वभौम है। दूसरे अर्थों में उसे मनुष्यता—मानवी गरिमा के अनुरूप उच्चस्तरीय श्रद्धा, सद्भावना कह सकते हैं। इसके प्रकाश में मनुष्य परस्पर स्नेह-सौजन्य के बन्धनों में बंधते हैं। सहिष्णु बनते हैं। एक-दूसरे के निकट आते और समझने का प्रयत्न करते हैं। विभेद की खाई पाटते हैं, पर सभ्यताओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे क्षेत्रों-जातियों, मान्यताओं और परिस्थितियों का कलेवर ओढ़े रहने से स्पष्टतः एक दूसरे से बहुत हद तक पृथक दीखती है और कितनी ही बातों में उनके बीच साधारण मतभेद भी है। सभ्यताएं टकराती हैं। एक सभ्यता के अनुयायी दूसरे लोगों को अपने झन्डे के तले लाने के लिए उचित ही नहीं अनुचित उपाय भी काम में लाते हैं। अपनी सभ्यता को दूसरों की सभ्यता के आक्रमण से बचाने के लिए लोग सुरक्षा के लिए भारी प्रयत्न करते हैं। ऐसे उपाय सोचते हैं जिनसे परस्पर घुलने-मिलने और आदान-प्रदान के अवसर न आने पावें। धर्मों के बीच कट्टरता इस हद तक देखी जाती है कि दूसरे धर्म के पूजा उपचारों में सम्मिलित होने पर भी प्रतिबन्ध रहता है। इसी प्रकार एक सभ्यता वाले अपने लोगों को दूसरी सभ्यता वालों के वेष विन्यास तक को अस्वीकार करते हैं। विचारों की तुलनात्मक समीक्षा करने की तो उनमें गुंजाइश ही नहीं रहती। अपना सो सर्वश्रेष्ठ, दूसरों का सो निकृष्टतम। यही अहंकार बुरी तरह छाया रहता है। सभ्यतानुयायी और धर्मावलम्बी कहलाने वाले व्यक्ति ही इस पक्षपात के सर्वाधिक शिकार पाये जाते हैं।
संस्कृति सौन्दर्योपासना है। एक भावभरी उदात्त दृष्टि रहे। वन, उपवनों, नदी, तालाबों प्राणियों, बादलों तारकों जैसी सामान्य वस्तुओं को जब सौन्दर्य पारखी दृष्टि से देखा जाता है तो वे अन्तरात्मा में आह्लाद उत्पन्न करती हैं। श्रद्धा के आरोप से पत्थर में भगवान पैदा होते हैं। सांस्कृतिक चिन्तन से हम इस संसार को भगवान का विराट स्वरूप और अपने कलेवर को ईश्वर के मन्दिर जैसा पवित्र अनुभव कर सकते हैं। जहां ऐसी दृष्टि होगी वहां दूसरों से सद्व्यवहार करने और अपनी उत्कृष्टता बनाये रखने की ही आकांक्षा बनी रहेगी और उसे जितना कार्यान्वित करना बन पड़ेगा, उतना ही अपना और दूसरों का सच्चा हित साधन बन पड़ेगा। सुसंस्कृत दृष्टिकोण अपनाकर मनुष्य अपने देवत्व को विकसित करने और वातावरण को सुख-शान्ति से भरा-पूरा बनाने में आशाजनक सफलता प्राप्त कर सकता है।
विचारक इलियट ने अपने ग्रन्थ ‘संस्कृति का पर्यवेक्षण’ में लिखा है—संस्कृति का स्वरूप मानवी उत्कृष्टता के अनुरूप आचरण करने के लिए विवश करने वाली आस्था है। जिसका अन्तःकरण इस रंग में जितनी गहराई तक रंगा हुआ है वह उतना ही सुसंस्कृत हैं।
धर्म का मर्म-आस्थाओं में परिवर्तन लाना—
विज्ञान ने इस मान्यता को इतना उलझा दिया है कि आज संसार में सर्वत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विश्रंखलता व्याप्त हो गई है। विराट दृष्टि से विचार करने पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और दिखाई देता है पर तत्काल लाभ की दृष्टि से कुछ और दिखाई देता है पर तत्काल लाभ की दृष्टि से कुछ और। विज्ञान ने इस स्थिति में पर्यवेक्षक बनकर मनुष्य को अनजान वन में भटका दिया है विचार करके भी मनुष्य उससे लौट कर अपने यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहा।
अच्छा करना तभी सम्भव हो सकता है, जब उसके मूल में अच्छा चिन्तन भी उत्कृष्टता की प्रेरणा भरता रहे। करना मूल्यवान है, पर सोचना अव्यक्त होते हुए भी क्रिया-कलाप के समतुल्य ही महत्वपूर्ण है। लोगों को श्रेष्ठ काम करने के लिए कहा जाय, पर साथ ही उन्हें यह भी सुझाया जाय कि कर्म का बाह्य स्वरूप ही सब कुछ नहीं है, उसकी आत्मा तो उद्देश्यों में निवास करती है।
अन्तर्राष्ट्रीय मसीही धर्म सम्मेलन में उद्बोधन करते हुए संसार के ईसाई जगद्गुरु-आर्कविशप कार्डिनल ग्रासीयास ने कहा था—मसीही धर्म समेत समस्त धर्मावलम्बियों को अपने सहयोग का क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक बनाना चाहिए। यह सहयोग पारस्परिक सद्भाव सहानुभूति और विश्वास पर आधारित होना चाहिये। धर्म की मूल धारणा और ईश्वर प्रदत्त न्याय की समूची परम्परा की रक्षा, उसका विकास और उसे समृद्ध बनाने जैसे महान् कार्यों में विभिन्न धर्म मिल-जुलकर काम कर सकते हैं।
अनास्था का संकट सभी धर्मों के सामने समान रूप से है। उद्योग, विज्ञान और विकृत तर्कवाद ने जो अनास्था उत्पन्न की है, उससे प्रभावित हुए बिना कोई धर्म रहा नहीं है। संचित कुसंस्कारों की, पशु प्रवृत्तियों को इस अनास्था ने और भी भड़काया है, फलतः समूची मनुष्य जाति स्वार्थान्धता और दुष्टता की काली छाया से ग्रसित होती चली जा रही है।
धर्म का तात्पर्य है—शालीनता एवं नीति मत्ता। यह प्रयोजन उच्चस्तरीय आस्थाओं के सहारे ही सधता है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रिया कृत्य के साथ सज्जनता और उदारता के तत्वों को संजो देने की विचार पद्धति का नाम अध्यात्म है। आध्यात्मिकता का चक्र आस्तिकता की धुरी के इर्द-गिर्द घूमता है इन सबका परस्पर सम्बन्ध और तारतम्य है। एक कड़ी तोड़ देने से यह समूची जंजीर ही बिखर जाती है। वैयक्तिक जीवन में जिसे नीतिमत्ता कहते हैं, वही सामूहिक रूप में विकसित होने के उपरान्त सामाजिक सुव्यवस्था बन जाती है। प्रगति और समृद्धि की सुख और शान्ति की आधार शिला इसी पृष्ठभूमि पर रखी जाती है।
नीति क्या है? इसका उत्तर उतना सरल नहीं है जितना कि समझा जाता है। उसका स्वरूप कई विचारक कई तरह प्रस्तुत करते हैं। नीति शास्त्री सिज्विक ने अपने ग्रन्थ ‘‘मैथड आफ एथिक्स’’ में लिखा है सत्य बोलना अपरिहार्य नहीं है। राज पुरुषों को अपनी गतिविधियां गुप्त रखनी पड़ती हैं। व्यापारियों को भी अपने निर्माण तथा विक्रय के रहस्य छिपाकर रखने पड़ते हैं। अपराधों को पकड़ने के लिये जासूसी की कला नितान्त उपयोगी है उसमें दुराव और छल का प्रश्रय लिया जाता है। इसलिए नीति का आधार सचाई को मानकर नहीं चला जा सकता। अधिक लोगों के अधिक सुख का ध्यान रखते हुए नीति का निर्धारण होना चाहिए।
लेस्ले स्टीफन ने अपने ग्रन्थ ‘साइन्स आफ एथिक्स’ में लिखा है—किसी के कार्य के स्वरूप को देखकर उसे नीति या अनीति की संज्ञा देना उचित नहीं। कर्त्ता की नीयत और कर्म के परिणाम की विवेचना करने पर ही उसे जाना जा सकता है।
क्रिया कृत्यों को देखकर नीतिमत्ता का निर्णय नहीं हो सकता। सम्भव है कोई व्यक्ति भीतर से छली होकर भी बाहर से धार्मिकता का आवरण ओढ़े हो, यह भी हो सकता है कि कोई धर्म कृत्यों से उदासीन रहकर भी चरित्र और चिन्तन की दृष्टि से बहुत ऊंची स्थिति में रह रहा हो। व्यक्ति की गरिमा, मात्र उसकी आन्तरिक आस्थाओं को देखने से ही जानी जा सकती है। नीयत ऊंची रहने पर यदि व्यवहार में भूल या भ्रम से कोई ऐसा काम बन पड़े जो देखने वालों को अच्छा न लगे, तो भी यथार्थता जहां की तहां रहेगी। अव्यवस्था फैलाने के लिए उसे दोषी समझा और दण्डित किया जा सकता है। इतने पर भी उसकी उत्कृष्टता अक्षुण्य बनी रहेगी। व्यक्तित्व और कर्तव्य की सच्ची परख उसकी आस्थाओं को समझे बिना हो नहीं सकती। धर्म तत्व की गहन गति इसीलिए मानी गई है कि उसे मात्र क्रिया के आधार पर नहीं जाना जा सकता। नीयत या ईमान ही उसका प्राण भूत मध्य बिन्दु है।
संस्कृत का अर्थ है—सुसंस्कारिता। इसके पर्यायवाची शब्द हैं—सज्जनता और आत्मीयता। ऐसी आत्मीयता जो दूसरों के सुख-दुःख को अपनी निजी सम्वेदनाओं का अंग बना सके। यह सार्वभौम और सर्वजनीन है। संस्कृति के खण्ड नहीं हो सकते उसे जातियों, वर्गों, देशों और सम्प्रदायों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यदि संस्कृति को वर्गहित के साथ जोड़ दिया गया तो वह मात्र विजेताओं और शक्तिमन्तों की ही इच्छा पूरी करेगी। अन्य लोग तो उससे पिसते और पददलित ही होते रहेंगे। ऐसी संस्कृति को विकृति ही कहा जायगा भले ही उसे लवादा कितना ही आकर्षक क्यों न पहनाया गया हो।
संस्कृति एक है उसे खण्डों में विभक्त नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा वह टुकड़े आपस में टकराने लगेंगे और जादवी वंश विनाश का अप्रिय प्रसंग उपस्थित करेंगे जर्मन संस्कृति, अरब संस्कृति, रोम संस्कृति आदि के पक्षधरों ने अपने अत्युत्साह को उस चौराहे पर इस तरह नंगा ला खड़ा किया जहां विश्व संस्कृति की आत्मा को अपनी लज्जा बचानी कठिन पड़ गई। सर्वहारा को निवोदित संस्कृति, सामान्य जन-जीवन को मानवोचित न्याय प्राप्त कर सकने का अवसर दे सकेगी इसमें सन्देहों की भरमार होती चली जा रही है। माओ की लाल किताब में वह आह्वान छपा है जिसमें कहा गया है कि हिमालय की चोटी पर खड़ा माओ ऐशिया को अपने पास बुला रहा है। उस आमन्त्रण को जिन्हें स्वीकार करना है सोचते हैं निकट बुलाने के उपरान्त आखिर हमारा किया क्या जायगा?
विचारों का एकाकी प्रवाह सदा उपयोगी ही नहीं होता उसमें बहुधा एक पक्षीय विचारणा का बाहुल्य जुड़ जाने से यथार्थता की मात्रा घटने लगती है। अपनी मान्यता और आकांक्षा के पक्ष में मस्तिष्क काम करता चला जाता है और प्रतिपक्षी तर्कों एवं तथ्यों का ध्यान ही नहीं रहता। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी तर्कों को सामने रखा जाना चाहिए। न्यायाधीश को वस्तुस्थिति समझने के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के प्रमाण, साक्षी एवं तर्क सुनने पड़ते हैं। अन्य न्यायाधीशों ने ऐसे प्रसंगों पर क्या-क्या निष्कर्ष निकाले हैं इसका ध्यान रखना पड़ता है। तब कहीं उचित निर्णय करने की स्थिति बनती है। यदि एक ही पक्ष की बात सुनी जाय दूसरा पक्ष कुछ बताये ही नहीं तो स्वभावतः एकांगी निर्णय करने की स्थिति खड़ी हो जायगी। इसमें न्याय के स्थान पर अन्याय का पक्षपात जैसी दुर्घटना घटित हो जायगी। इसमें न्यायाधीश की नीयत का नहीं उस एकांगी परिस्थिति का दोष है जिसमें मन्थन के लिए—काट-छांट के लिए अवसर ही नहीं मिला और न करने योग्य निर्णय कर लिया गया। यही दुर्घटना तब घटित होती है जब एकांगी-एक पक्षीय-विचारों की घुड़दौड़ मस्तिष्क में चलती रहती है और ऐसे निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं जो अनुपयुक्त होने के कारण असफल एवं उपहासास्पद सिद्ध होते हैं।
यदि मन पक्षपाती पूर्वाग्रहों से भरा हो तो फिर आप्त वचन और शास्त्र भी सही मार्गदर्शन कर सकने में असमर्थ रहेंगे। उनकी व्याख्याएं इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर की जाने लगेंगी कि तर्क की दृष्टि से उस प्रतिपादन को चमत्कारी माना जायगा फिर भी शास्त्रकारों और आप्त पुरुषों के मूल मन्तव्य की वास्तविकता के साथ उसकी पटरी बिठाना अति कठिन हो जायगा।
गीतों के अनेकों भाष्य हुए हैं। इन भाष्यकारों ने जो भाष्य किये हैं उनमें उनका अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने का आग्रह ही प्रधान रूप से काम करता है। जान-बूझकर अथवा अनजाने ही वे मूल ग्रन्थकार के वास्तविक उद्देश्य के विपरीत बहुत दूर तक निकल गये हैं। यदि ऐसा न होता तो इतने तरह के परस्पर विरोधी भाष्य एक ही ग्रन्थ के क्योंकर लिखे जा सकते? इनमें से कुछ ही टीकाकार सही हो सकते हैं। कर्त्ता का यह उद्देश्य तो रहा नहीं होगा कि वह ऐसी वस्तु रच दे जिसका तात्पर्य निकालने वाले इस प्रकार के परस्पर विरोधी जंजाल में फंसकर स्वयं भ्रमित हों और दूसरों को भ्रमित करें। रामायण की अनेक चौपाइयों के ऐसे विचित्र अर्थ सुनने में आते हैं जिन्हें यदि मूल रचनाकार के सामने रखा जाय तो स्वयं आश्चर्यचकित होकर रह जायेंगे कि जो बातें कल्पना में भी नहीं थीं वे उनके गले किस प्रकार मढ़ दी गईं।
संसार के मूर्धन्य साहित्यकारों के अपनी कृतियों में भारतीय शास्त्रों और मनीषियों के अनेकों उद्धरण दिये हैं। ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है कि उद्धरणों की शब्द रचना यथावत् है, किन्तु उन्हें इस प्रकार के प्रयोजनों में प्रयुक्त किया गया है जैसा कि उन कथनों का मूल उद्देश्य नहीं था। डी. एच. लारेन्स ने अपनी अन्तःस्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है—‘‘मेरे भीतर एक नहीं कई देवता निवास करते हैं।’’ यहां उनने देवताओं को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह देववाद के मूल प्रतिपादनों के अनुरूप नहीं हैं। हैनरी मिलर की पुस्तकों में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द के उद्धरणों की भरमार है, पर वे मूलतः उन मन्तव्यों के लिए नहीं कहे गये थे जैसा कि मिलर ने सिद्ध किया है। स्टेनबेक ने अपनी पुस्तक ‘केनेरी को’ में संस्कृत कवि विल्हण की कई रचनाओं का उल्लेख किया है। कालिन विल्सन ने मानवी पृथकतावाद के समर्थन में भारत में प्रचलित धर्म दृष्टान्तों का अनेक प्रसंगों में सहारा लिया है। आल्डुआस हक्सले ने प्राचीनता और आधुनिकता के विग्रह में भगवान बुद्ध को आधुनिकता का समर्थक सिद्ध किया है। एरिक फ्राम ने अपनी पुस्तक ‘आर्ट आफ लविंग’ में योरोप में उत्पन्न हुए अनेकों संघर्षों की जड़ अरस्तु के तर्क शास्त्र को बताया है जिसने जनमानस में यह बात बिताई कि संसार में देव और असुर दो ही शक्तियां हैं और दोनों परस्पर विरोधी हैं। यह (ए, एण्ड नान ए) का सिद्धान्त मुद्दतों तक लोगों के दिमागों में गूंजता रहा है और वे यह सोचते रहे कि बुराई पर आक्रमण करके उसे मिटाया जाना चाहिए। अब इसका निर्णय कौन करे कि बुराई किस पक्ष की है? अपनी या पराई? इस निष्कर्ष में फैसला अपने ही पक्ष को सही मानने की ओर झुकता है। हम जो सोचते और करते हैं वही ठीक है। गलती तो अन्य लोग ही कर सकते हैं, वह हमसे क्यों होगी? इसी पूर्वाग्रह से हर व्यक्ति और वर्ग घिरा रहता है। फलतः उसे सामने वाले में ही बुराई दीखती है और उसे मिटाने के लिए तलवार पर धार रखता है। इसी मान्यता ने कलह विद्वेष और आक्रमणों को जन्म दिया है।
उच्चस्तरीय आस्थाओं के प्रति व्यक्ति को निष्ठावान् बनाना अध्यात्मवादी तत्वदर्शन का काम है। धर्म और दर्शन का लक्ष्य यही है। संस्कृति की उपयोगिता इसी में है कि वहमानवी चिन्तन का स्तर ऊंचा उठाये। उसे आत्म गौरव की अनुभूति कराने के साथ-साथ सज्जनता को व्यवहार में उतारने का साहस भी प्रदान करे।
सत्य की उपेक्षा न हो—
आज विज्ञान को अनास्था का सेनापति बनाकर खड़ा कर दिया गया है और उसे विश्रंखित जीवन के सैनिकों की भर्ती करने की छूट दे दी गई है। फलस्वरूप सदाचरण जैसी मानवीय गरिमा आज औंधे मुंह पड़ी सिसक रही है। दूसरी ओर अवांछनीयता उच्छृंखलता का दानव सर्वत्र कबड्डी खेलता घूम रहा है।
अहंकार और व्यामोह का समन्वित रूप बनता है—दुराग्रह। इसमें आवेश और हठ दोनों ही जुड़े रहते हैं। फलतः चिन्तन तन्त्र के लिए यह कठिन पड़ता है कि वह सत्य और तथ्य को ठीक तरह समझ सके और उचित-अनुचित का भेद कर सके। अभ्यस्त मान्यताओं के प्रति एक प्रकार की कट्टरता जुड़ जाती है। इसे अच्छी तरह से सिद्ध करने के लिए परम्पराओं के निर्वाह की दुहाई दी जाती है। उसका समर्थन धर्मशास्त्र, आप्तवचन, देश भक्ति आदि के नाम पर किया जाता है और कई बार तो उसे ईश्वर का आदेश तक घोषित कर दिया जाता है।
अपना धर्म श्रेष्ठ दूसरे का निकृष्ट—अपनी जाति ऊंची दूसरे की नीची—अपनी मान्यता सच दूसरे की झूंठ—ऐसा दुराग्रह यदि आरम्भ से ही हो तो फिर सत्य असत्य का निर्णय हो ही नहीं सकता न्याय और औचित्य की रक्षा के लिए आवश्यक है कि तथ्यों को ढूंढ़ने के लिए खुला मस्तिष्क रखा जाय और अपने पराये का—नये पुराने का—भेदभाव न रखकर विवेक और तर्क का सहारा लेने की नीति अपनाई जाय। सत्य को प्राप्त करने का लक्ष्य इस नीति को अपनाने से पूरा हो सकता है। पक्षपात और दुराग्रह तो सत्य को समझने से इन्कार करना है। ऐसे हठी लोग प्रायः सत्य और सत्यशोधकों को सताने तक में नहीं चूकते।
टेलिस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो ने जब पृथ्वी को गतिशील बताने का सर्वप्रथम साहस किया तो पुरातन पंथी धर्म गुरुओं ने इसे धर्म विरुद्ध ठहराया। उसे तरह-तरह से सताया गया और जेल में बन्द करके सड़ाया गया। सबसे पहले जब पैरिस में रेलगाड़ी चली तो उस प्रचलन का पुरातन पंथियों ने घोर विरोध किया और कहा जो काम हमारे महान पूर्वज नहीं कर सके उन्हें करना अपने पूर्व पुरुषों के गौरव पर बट्टा लगाना है। रेलगाड़ी के चलाने वाले जोसफ केग्नार को उस जुर्म में जेल में डाला गया कि वह ईश्वर के नियमों के विरुद्ध काम करता है। इटली में शरीर शास्त्र की शिक्षा किसी समय अपराध थी। आपरेशन करना पाप समझा जाता था और कोई चिकित्सक छोटा-मोटा आपरेशन भी करता पाया जाता तो उसे मृत्यु दण्ड सुनाया जाता था।
कारीगर रैगर बेकन ने सर्वप्रथम दो कोनों को जोड़कर सूक्ष्म दर्शी यन्त्र बनाया था। इस आविष्कार की निन्दा की गई। उस कारीगर को इस खतरनाक काम को करने के अभियोग में दस वर्ष की कैद सुनाई गई। बेचारा जेल में ही तड़प-तड़प कर मर गया।
रसायन शास्त्र के कुछ नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के अपराध में स्वन्ति अरहीनियस को प्राध्यापक के पद से पदच्युत करके एक छोटा अध्यापक बनाया गया और उसे सनकी ठहराकर अपमानित किया गया। विधि का विधान ही समझिये कि वही सिद्धान्त आगे चलकर विज्ञान जगत में सर्वमान्य हुए और स्वन्ति को उन्हीं पर नोबेल पुरस्कार मिला।
डा. हार्ले ने जब सर्वप्रथम यह कहा कि रक्त नसों में भरा नहीं रहता वरन् चलता रहता है तो समकालीन चिकित्सकों ने उसे खुले आम बेवकूफ कहा। ब्रूनो ने जब अन्य ग्रहों पर भी जीवन होने की सम्भावना बताई तो लोग इतने क्रुद्ध हुए कि उसे जीवित ही जला दिया।
दुराग्रह के अत्याचारों का इतिहास बहुत लम्बा और बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। पिछले दिनों यह हठवादिता बहुत चलती रही है। धर्म परम्परा, देश भक्ति, ईश्वर का आदेश आदि न जाने क्या-क्या नाम इस हठवादिता को दिये जाते हैं। और सत्य एवं धर्म की आत्मा का हनन होता रहा है। मानवी विवेक में निष्पक्ष सत्यशोधक की दृष्टि को ही प्रश्रय मिलना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब धर्म आगे-आगे चले और विज्ञान तथ्यानुयायी बने।
संस्कृति का अर्थ है मनुष्य का भीतरी विकास। उसका परिचय व्यक्ति के निजी चरित्र और दूसरों के साथ किये जाने वाले सद्व्यवहार से मिलता है। दूसरों को ठीक तरह समझ सकने और अपनी स्थिति एवं समझ धैर्यपूर्वक दूसरों को समझा सकने की स्थिति भी उस योग्यता में सम्मिलित कर सकते हैं। जो संस्कृति की देन है।
आदान-प्रदान एक तथ्य है जिसके सहारे मानवी प्रगति के चरण आगे बढ़ते-बढ़ते वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। कृषि, पशु पालन शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, विज्ञान, दर्शन जैसे जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के सम्बन्धित प्रसंग किसी एक क्षेत्र या वर्ग की वपौती नहीं है। एक वर्ग की उपलब्धियों से दूसरे क्षेत्र के लोग परिचित हुए हैं। परस्पर आदान-प्रदान चले हैं और भौतिक क्षेत्र में सुविधा सम्वर्धन का पथ-प्रशस्त हुआ है। ठीक यही बात धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध में भी है। एक ने अपने सम्पर्क क्षेत्र को प्रभावित किया है। एक लहर ने दूसरी को आगे धकेला है। लेन-देन का सिलसिला सर्वत्र चलता रहा है। मिलजुल कर ही मनुष्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इस समन्वय से धर्म और संस्कृति भी अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित किया है।
अब दुनिया में कोई नस्ल ऐसी नहीं बची जो पूरी तरह रक्त शुद्धि का दावा कर सके। जातियों के बीच प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बेटी व्यवहार चलते रहे हैं और नस्लों के मूल रूप में आश्चर्य जनक परिवर्तन हो गया है। भारत वंशी लोगों के रक्त में आर्य और द्रविड़ रक्त का सम्मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि दोनों से मिलकर एक तीसरी अथवा संयुक्त जाति बन गई है। इसी प्रकार एक सभ्यता पर दूसरी सभ्यता के निकट आने का भारी प्रभाव पड़ा है। भारत में पिछले एक हजार वर्ष में मुस्लिम और ईसाई सभ्यताएं आती रही हैं। उनके पूर्ण अनुयायी कितने बने यह बात पृथक है। सामान्य जनमानस ने उनका बहुत कुछ प्रभाव ग्रहण किया है। प्रचलित भारतीय पोशाक ऐसी नहीं है। जिसे दो हजार वर्ष पुरानी कहा जा सके। इसी प्रकार रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं में भी अनजाने ऐसे तत्व का समावेश होता रहा है जिसे खुले मन से न सही हिचकिचाहट के साथ—समन्वय स्वीकार किया जा सके।
यह सभ्यताओं का समन्वय एवं आदान-प्रदान उचित भी है और आवश्यक भी। कट्टरता के कटघरे में मानवी विवेक को कैद रखे रहना असम्भव है। विवेक दृष्टि जागृत होते ही इन कटघरों की दीवारें टूटती हैं और जो रुचिकर या उपयोगी लगता है उसका बिना किसी प्रचार या दबाव के आदान-प्रदान चल पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए कट्टरपंथी प्रयास सदा से हाथ-पैर पीटते रहे हैं, पर यह कठिन ही रहा है। हवा उन्मुक्त आकाश में बहती है। सर्दी-गर्मी का विस्तार व्यापक क्षेत्र में होता है। इन्हें बन्धनों में बांधकर कैदियों की तरह अपने ही घर में रुके रहने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। सम्प्रदाओं और सभ्यताओं में भी यह आदान-प्रदान अपने ढंग से चुपके चुपके चलता रहा है। भविष्य में इसकी गति और भी तीव्र होगी।
धर्म और संस्कृति के बारे में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। वे दोनों ही सार्वभौम हैं उन्हें सर्वजनीन कहा जा सकता है। मनुष्यता के टुकड़े नहीं हो सके। सज्जनता की परिभाषा में बहुत मतभेद नहीं है। शारीरिक संरचना की तरह मानवी अन्तःकरण की मूल सत्ता भी एक ही प्रकार की है भौतिक प्रवृत्तियां भी लगभग एक-सी हैं। एकता व्यापक है और शाश्वत। पृथकता सामयिक है और क्षणिक। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। एक ही धरती पर पैदा हुए हैं। एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। एक ही सूर्य से गर्मी पाते हैं और बादलों के अनुदार से एक ही तरह अपना गुजारा करते हैं फिर कृत्रिम विभेद से बहुत दिनों तक बहुत दूरी तक किस प्रकार बंधे रह सकते हैं। औचित्य को आधार मानकर परस्पर आदान-प्रदान का द्वार जितना खोलकर रखा जायगा उतना ही स्वच्छ हवा और रोशनी का लाभ मिलेगा। खिड़कियां बन्द रखकर हम अपनी विशेषताओं को न तो सुरक्षित रख सकते हैं और न स्वच्छ हवा और खुल धूप से मिलने वाले लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। संकीर्णता अपना कर पाया कम, और खोया अधिक जाता है। एकता की दिशा में हम आगे बढ़ें तो इसमें पूर्वजों के प्रति अनास्था नहीं वरन् श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति है। पूर्वज अपने पूर्वजों की विरासत को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए भी अपने बुद्धिबल और बाहुबल से नये अनुभव एकत्रित करते, लाभ कमाते और साधन जुटाते रहे हैं। इसमें पूर्वजों को सन्तोष ही हो सकता है। साथ ही गर्व भी। अपनी संतान पर कोई अभिभावक यह बन्धन नहीं लगाता कि हममें अधिक शिक्षा या सम्पत्ति सन्तान को नहीं कमानी चाहिए। हममें अधिक यश या कौशल अर्जित नहीं करना चाहिए। बन्धन लगाना तो दूर—समझदार अभिभावक अपने से अधिक प्रगति करने के लिए अपने उत्तराधिकारियों को उत्साहित और उत्तेजित करते हैं। ऐसी दशा में पूर्वजों की तुलना में एकता के क्षेत्र में हम कुछ कदम और आगे बढ़ सके तो इसमें असमंजस की कोई बात नहीं है। इसमें पूर्वजों की अवज्ञा जैसी कोई प्रश्न उठता नहीं नहीं। पिताजी यदि 60 वर्ष जियें और बेटा 70 वर्ष जी सके तो इसमें दुःख मानने की कोई बात नहीं है। सदाशयता, शालीनता, एकता और विवेकशीलता की दिशा में प्रगति करना मानवी प्रगति के इतिहास में एक अच्छी कड़ी और जोड़ देना ही कहा जा सकता है।
अब राष्ट्रवाद के दिन लदते जा रहे हैं। देशभक्ति के जोश को अब उतना नहीं उभारा जाता जिसमें अपने ही क्षेत्र या वर्ग को सर्वोच्च ठहराया जाय अथवा विश्व विजय करके सर्वत्र अपना ही झण्डा फहराने का उन्माद उठ खड़ा हो। ऐसी पक्षपाती और आवेशग्रसित देशभक्ति अब विचारशील वर्ग में नापसन्द की जाती है और विश्व नागरिकता की वसुधैव कुटुम्बकम् की बात को महत्व दिया जाता है। विश्व एकता के सिद्धान्त को मान्यता मिली है और राष्ट्र संघ बना है। इस दिशा में प्रगति के चरण धीमे उठ रहे हैं, यह चिन्ता का प्रसंग है। अपेक्षा यही की जाती है कि संसार की व्यापक समस्याओं का समाधान विश्व एकता के बिना और किसी प्रकार सम्भव न हो सकेगा। एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति अपना कर ही उज्ज्वल भविष्य की, विश्व शान्ति की स्थापना हो सकती है। यह तथ्य मानवी विवेक ने स्वीकार कर लिया है और विभेद उभारने वाले तत्वों को अमान्य ठहराया जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी ऐसी ही व्यापक एकता उत्पन्न करने के लिए वातावरण बनाना होगा। राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद की तरह सभ्यतावाद की कट्टरता को भी अगले दिनों क्रमशः अधिक शिथिल करते चलने की आवश्यकता पड़ेगी। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए ऐसे एकतावादी विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है जिसमें अपने ही पक्ष को सर्वोपरि ठहराये जाने का आग्रह न हो। अपने पराये का भेदभाव न करके औचित्य, न्याय तथ्य और विवेक को ही जब मान्यता दी जायगी तो फिर उपयोगिता स्वीकार करने की मनःस्थिति बन जायगी तब जहां से भी—जितनी मात्रा में तथ्य दृष्टिगोचर होगा स्वीकार किया जायगा। इसके लिए किसी को खेद मनाने की आवश्यकता न होगी कि हमारी अमुक मान्यताओं को सर्वाश में जागृत विवेक ने स्वीकार नहीं किया। पिछला पैर उठाकर ही अगला पैर आगे रखा जाता है। लम्बी मंजिल इसी प्रकार पूरी होती है। आगे बढ़ना है तो पीछे का पैर अपने स्थान पर जमाये रहने का अग्रह नहीं चल सकता।
अंग्रेजी में संस्कृति का अर्थ बोधक शब्द है ‘कलचर’ इसका तात्पर्य है—सभ्यता। रहन-सहन एवं सोचने विचारने का तरीका। अपने नाम, रूप, धन, परिवार, क्षेत्र, भाषा, धर्म आदि की तरह ही अपने रहन-सहन की पद्धति भी लोगों को प्रिय लगती है। यह प्रियता बहुधा पक्षपात के रूप में बदल जाती है। जो अपने को श्रेष्ठ दूसरों को निकृष्ट मानने की तरह है। अपने परिकर एवं सरंजाम के सम्बन्ध में भी वैसी ही मान्यता बन जाती है। इसमें पूर्वाग्रह और पक्षपात का गहरा पुट रहता है। यद्यपि वह लगता ऐसा है मानो सत्य अपने ही हिस्से में आया है। और दूसरे सभी गलत सोचते और झूठ बोलते हैं। अन्यान्य मतभेदों की तरह संस्कृति सम्बन्धी मतभेद भी एक है जिसके लिए बहुत बार भयंकर युद्ध होते रहे। व्यक्तिगत जीवन में भी विद्वेष, घृणा, आक्रमण, प्रतिरक्षा जैसी विडम्बनाएं अनेक बार संस्कृति के नाम पर भी खड़ी होती रही हैं। और उनसे मनुष्य जाति को धन, जन, नीति, सद्भावना, शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से भारी हानि उठानी पड़ी है। इस प्रकार जहां संस्कृति का मूल अस्तित्व व्यक्ति और समाज के कल्याणकारी तत्व पर आधारित है वहां उसके प्रति अत्युत्साह और दुराग्रह में विद्वेष के विष बीज भी कम मात्रा में भरे हुए नहीं हैं। योरोप में ईसाई धर्म के प्रति और एशिया में इस्लाम धर्म के प्रति अत्युत्साह ने जिस निष्ठुरता का परिचय दिया है, उससे उन संस्कृति प्रेमियों का गौरव बढ़ा नहीं। उन धर्मों की गरिमा अन्तःकरण की गहराई में प्रवेश न कर सकी यद्यपि बहुतों ने भयभीत होकर अथवा लोभ लाभ की दृष्टि से उन्हें स्वीकार अवश्य कर लिया।
संस्कृति शब्द को सभ्यता से पृथक रखा जा सके तो अर्थ का अनर्थ होने से बच सकता है। धर्म और सम्प्रदाय के सम्बन्ध में भी यही बात होनी चाहिए। धर्म एक चीज है और सम्प्रदाय दूसरी। सम्प्रदायवाद-धर्म तत्व का समर्थक ही हों यह आवश्यक नहीं। बहुत-सी रिवाजें एवं मान्यताएं ऐसी हो सकती हैं जो प्राचीन होने के साथ-साथ लोक प्रिय बन गई हों और अनेकों व्यक्ति उसके समर्थक अनुयायी हों, इतने पर भी उनका बहुत-सा पक्ष, धर्म भावना के मूल सिद्धान्तों से मेल न खाता हो। भारतीय समाज को ही लें। जाति-पांति के नाम पर ऊंच-नीच की भावना और नर-नारी की असमानता की मान्यता गहराई तक लोगों के मनों में उतर गई है। नीति और न्याय की दृष्टि से उसका तनिक भी औचित्य नहीं है। फिर भी परम्परागत अभ्यास के कारण उसकी जड़ें इतनी नीची चली गई हैं की काटे नहीं कटती। इसी प्रकार हिन्दू धर्म में अथवा अन्य धर्मों में ऐसे ही प्रचलन हो सकते हैं। देवताओं के सामने पशु बलि चढ़ाया जाना, धर्म की मूल मान्यताओं से, उच्चस्तरीय आदर्शों से मेल नहीं खाता फिर भी उसे अनेक धर्मों में मान्यता प्राप्त है।
जिस प्रकार सम्प्रदाय को धर्म का कलेवर भर कह सकते हैं वैसे ही सभ्यताओं में संस्कृति के कुछ तत्व झांकते हुए देखे जा सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, वेश-विन्यास देख कर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती हैं फिर भी उस आवरण को पूरा व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। धर्म एक तत्वज्ञान है जिसमें उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श कर्तृत्व की दिशा में मनुष्य को अग्रगामी बनाने के लिए कुछ नीति-नियमों का निर्धारण है। सम्प्रदाय उस दृष्टिकोण को मानने वाले समुदाय के रहन-सहन का तरीका है। यह तरीका मात्र आदर्शों से ही प्रेरित नहीं होता वरन् परिस्थितियों, साधनों एवं परम्पराओं पर आधारित होता है। उसमें तत्व के सिद्धान्त भी किसी मात्रा में घुले-मिले हो सकते हैं, पर कोई समूचा सम्प्रदाय समूचे धर्म तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उसमें दूसरी चीजों का भी समावेश हो सकता है। किसी सम्प्रदाय का कट्टर अनुयायी सच्चे अर्थों में धर्मात्मा भी होगा यह नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार अनेकानेक सभ्यताओं में भी मानवी संस्कृति की झलक मिल सकती है पर कोई सभ्यता पूरी तरह सुसंस्कृत होने का दावा नहीं कर सकती। यदि ऐसा ही होता तो फिर पृथकता से लेकर विरोध तक के ऐसे तत्व कहीं दिखाई न पड़ते जिनसे टकराव की स्थिति पैदा होती हो।
संस्कृति देश और जाति में विभाजित नहीं हो सकती। वह मानवी है और सार्वभौम है। दूसरे अर्थों में उसे मनुष्यता—मानवी गरिमा के अनुरूप उच्चस्तरीय श्रद्धा, सद्भावना कह सकते हैं। इसके प्रकाश में मनुष्य परस्पर स्नेह-सौजन्य के बन्धनों में बंधते हैं। सहिष्णु बनते हैं। एक-दूसरे के निकट आते और समझने का प्रयत्न करते हैं। विभेद की खाई पाटते हैं, पर सभ्यताओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे क्षेत्रों-जातियों, मान्यताओं और परिस्थितियों का कलेवर ओढ़े रहने से स्पष्टतः एक दूसरे से बहुत हद तक पृथक दीखती है और कितनी ही बातों में उनके बीच साधारण मतभेद भी है। सभ्यताएं टकराती हैं। एक सभ्यता के अनुयायी दूसरे लोगों को अपने झन्डे के तले लाने के लिए उचित ही नहीं अनुचित उपाय भी काम में लाते हैं। अपनी सभ्यता को दूसरों की सभ्यता के आक्रमण से बचाने के लिए लोग सुरक्षा के लिए भारी प्रयत्न करते हैं। ऐसे उपाय सोचते हैं जिनसे परस्पर घुलने-मिलने और आदान-प्रदान के अवसर न आने पावें। धर्मों के बीच कट्टरता इस हद तक देखी जाती है कि दूसरे धर्म के पूजा उपचारों में सम्मिलित होने पर भी प्रतिबन्ध रहता है। इसी प्रकार एक सभ्यता वाले अपने लोगों को दूसरी सभ्यता वालों के वेष विन्यास तक को अस्वीकार करते हैं। विचारों की तुलनात्मक समीक्षा करने की तो उनमें गुंजाइश ही नहीं रहती। अपना सो सर्वश्रेष्ठ, दूसरों का सो निकृष्टतम। यही अहंकार बुरी तरह छाया रहता है। सभ्यतानुयायी और धर्मावलम्बी कहलाने वाले व्यक्ति ही इस पक्षपात के सर्वाधिक शिकार पाये जाते हैं।
संस्कृति सौन्दर्योपासना है। एक भावभरी उदात्त दृष्टि रहे। वन, उपवनों, नदी, तालाबों प्राणियों, बादलों तारकों जैसी सामान्य वस्तुओं को जब सौन्दर्य पारखी दृष्टि से देखा जाता है तो वे अन्तरात्मा में आह्लाद उत्पन्न करती हैं। श्रद्धा के आरोप से पत्थर में भगवान पैदा होते हैं। सांस्कृतिक चिन्तन से हम इस संसार को भगवान का विराट स्वरूप और अपने कलेवर को ईश्वर के मन्दिर जैसा पवित्र अनुभव कर सकते हैं। जहां ऐसी दृष्टि होगी वहां दूसरों से सद्व्यवहार करने और अपनी उत्कृष्टता बनाये रखने की ही आकांक्षा बनी रहेगी और उसे जितना कार्यान्वित करना बन पड़ेगा, उतना ही अपना और दूसरों का सच्चा हित साधन बन पड़ेगा। सुसंस्कृत दृष्टिकोण अपनाकर मनुष्य अपने देवत्व को विकसित करने और वातावरण को सुख-शान्ति से भरा-पूरा बनाने में आशाजनक सफलता प्राप्त कर सकता है।
विचारक इलियट ने अपने ग्रन्थ ‘संस्कृति का पर्यवेक्षण’ में लिखा है—संस्कृति का स्वरूप मानवी उत्कृष्टता के अनुरूप आचरण करने के लिए विवश करने वाली आस्था है। जिसका अन्तःकरण इस रंग में जितनी गहराई तक रंगा हुआ है वह उतना ही सुसंस्कृत हैं।
धर्म का मर्म-आस्थाओं में परिवर्तन लाना—
विज्ञान ने इस मान्यता को इतना उलझा दिया है कि आज संसार में सर्वत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विश्रंखलता व्याप्त हो गई है। विराट दृष्टि से विचार करने पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और दिखाई देता है पर तत्काल लाभ की दृष्टि से कुछ और दिखाई देता है पर तत्काल लाभ की दृष्टि से कुछ और। विज्ञान ने इस स्थिति में पर्यवेक्षक बनकर मनुष्य को अनजान वन में भटका दिया है विचार करके भी मनुष्य उससे लौट कर अपने यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहा।
अच्छा करना तभी सम्भव हो सकता है, जब उसके मूल में अच्छा चिन्तन भी उत्कृष्टता की प्रेरणा भरता रहे। करना मूल्यवान है, पर सोचना अव्यक्त होते हुए भी क्रिया-कलाप के समतुल्य ही महत्वपूर्ण है। लोगों को श्रेष्ठ काम करने के लिए कहा जाय, पर साथ ही उन्हें यह भी सुझाया जाय कि कर्म का बाह्य स्वरूप ही सब कुछ नहीं है, उसकी आत्मा तो उद्देश्यों में निवास करती है।
अन्तर्राष्ट्रीय मसीही धर्म सम्मेलन में उद्बोधन करते हुए संसार के ईसाई जगद्गुरु-आर्कविशप कार्डिनल ग्रासीयास ने कहा था—मसीही धर्म समेत समस्त धर्मावलम्बियों को अपने सहयोग का क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक बनाना चाहिए। यह सहयोग पारस्परिक सद्भाव सहानुभूति और विश्वास पर आधारित होना चाहिये। धर्म की मूल धारणा और ईश्वर प्रदत्त न्याय की समूची परम्परा की रक्षा, उसका विकास और उसे समृद्ध बनाने जैसे महान् कार्यों में विभिन्न धर्म मिल-जुलकर काम कर सकते हैं।
अनास्था का संकट सभी धर्मों के सामने समान रूप से है। उद्योग, विज्ञान और विकृत तर्कवाद ने जो अनास्था उत्पन्न की है, उससे प्रभावित हुए बिना कोई धर्म रहा नहीं है। संचित कुसंस्कारों की, पशु प्रवृत्तियों को इस अनास्था ने और भी भड़काया है, फलतः समूची मनुष्य जाति स्वार्थान्धता और दुष्टता की काली छाया से ग्रसित होती चली जा रही है।
धर्म का तात्पर्य है—शालीनता एवं नीति मत्ता। यह प्रयोजन उच्चस्तरीय आस्थाओं के सहारे ही सधता है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रिया कृत्य के साथ सज्जनता और उदारता के तत्वों को संजो देने की विचार पद्धति का नाम अध्यात्म है। आध्यात्मिकता का चक्र आस्तिकता की धुरी के इर्द-गिर्द घूमता है इन सबका परस्पर सम्बन्ध और तारतम्य है। एक कड़ी तोड़ देने से यह समूची जंजीर ही बिखर जाती है। वैयक्तिक जीवन में जिसे नीतिमत्ता कहते हैं, वही सामूहिक रूप में विकसित होने के उपरान्त सामाजिक सुव्यवस्था बन जाती है। प्रगति और समृद्धि की सुख और शान्ति की आधार शिला इसी पृष्ठभूमि पर रखी जाती है।
नीति क्या है? इसका उत्तर उतना सरल नहीं है जितना कि समझा जाता है। उसका स्वरूप कई विचारक कई तरह प्रस्तुत करते हैं। नीति शास्त्री सिज्विक ने अपने ग्रन्थ ‘‘मैथड आफ एथिक्स’’ में लिखा है सत्य बोलना अपरिहार्य नहीं है। राज पुरुषों को अपनी गतिविधियां गुप्त रखनी पड़ती हैं। व्यापारियों को भी अपने निर्माण तथा विक्रय के रहस्य छिपाकर रखने पड़ते हैं। अपराधों को पकड़ने के लिये जासूसी की कला नितान्त उपयोगी है उसमें दुराव और छल का प्रश्रय लिया जाता है। इसलिए नीति का आधार सचाई को मानकर नहीं चला जा सकता। अधिक लोगों के अधिक सुख का ध्यान रखते हुए नीति का निर्धारण होना चाहिए।
लेस्ले स्टीफन ने अपने ग्रन्थ ‘साइन्स आफ एथिक्स’ में लिखा है—किसी के कार्य के स्वरूप को देखकर उसे नीति या अनीति की संज्ञा देना उचित नहीं। कर्त्ता की नीयत और कर्म के परिणाम की विवेचना करने पर ही उसे जाना जा सकता है।
क्रिया कृत्यों को देखकर नीतिमत्ता का निर्णय नहीं हो सकता। सम्भव है कोई व्यक्ति भीतर से छली होकर भी बाहर से धार्मिकता का आवरण ओढ़े हो, यह भी हो सकता है कि कोई धर्म कृत्यों से उदासीन रहकर भी चरित्र और चिन्तन की दृष्टि से बहुत ऊंची स्थिति में रह रहा हो। व्यक्ति की गरिमा, मात्र उसकी आन्तरिक आस्थाओं को देखने से ही जानी जा सकती है। नीयत ऊंची रहने पर यदि व्यवहार में भूल या भ्रम से कोई ऐसा काम बन पड़े जो देखने वालों को अच्छा न लगे, तो भी यथार्थता जहां की तहां रहेगी। अव्यवस्था फैलाने के लिए उसे दोषी समझा और दण्डित किया जा सकता है। इतने पर भी उसकी उत्कृष्टता अक्षुण्य बनी रहेगी। व्यक्तित्व और कर्तव्य की सच्ची परख उसकी आस्थाओं को समझे बिना हो नहीं सकती। धर्म तत्व की गहन गति इसीलिए मानी गई है कि उसे मात्र क्रिया के आधार पर नहीं जाना जा सकता। नीयत या ईमान ही उसका प्राण भूत मध्य बिन्दु है।
संस्कृत का अर्थ है—सुसंस्कारिता। इसके पर्यायवाची शब्द हैं—सज्जनता और आत्मीयता। ऐसी आत्मीयता जो दूसरों के सुख-दुःख को अपनी निजी सम्वेदनाओं का अंग बना सके। यह सार्वभौम और सर्वजनीन है। संस्कृति के खण्ड नहीं हो सकते उसे जातियों, वर्गों, देशों और सम्प्रदायों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यदि संस्कृति को वर्गहित के साथ जोड़ दिया गया तो वह मात्र विजेताओं और शक्तिमन्तों की ही इच्छा पूरी करेगी। अन्य लोग तो उससे पिसते और पददलित ही होते रहेंगे। ऐसी संस्कृति को विकृति ही कहा जायगा भले ही उसे लवादा कितना ही आकर्षक क्यों न पहनाया गया हो।
संस्कृति एक है उसे खण्डों में विभक्त नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा वह टुकड़े आपस में टकराने लगेंगे और जादवी वंश विनाश का अप्रिय प्रसंग उपस्थित करेंगे जर्मन संस्कृति, अरब संस्कृति, रोम संस्कृति आदि के पक्षधरों ने अपने अत्युत्साह को उस चौराहे पर इस तरह नंगा ला खड़ा किया जहां विश्व संस्कृति की आत्मा को अपनी लज्जा बचानी कठिन पड़ गई। सर्वहारा को निवोदित संस्कृति, सामान्य जन-जीवन को मानवोचित न्याय प्राप्त कर सकने का अवसर दे सकेगी इसमें सन्देहों की भरमार होती चली जा रही है। माओ की लाल किताब में वह आह्वान छपा है जिसमें कहा गया है कि हिमालय की चोटी पर खड़ा माओ ऐशिया को अपने पास बुला रहा है। उस आमन्त्रण को जिन्हें स्वीकार करना है सोचते हैं निकट बुलाने के उपरान्त आखिर हमारा किया क्या जायगा?
विचारों का एकाकी प्रवाह सदा उपयोगी ही नहीं होता उसमें बहुधा एक पक्षीय विचारणा का बाहुल्य जुड़ जाने से यथार्थता की मात्रा घटने लगती है। अपनी मान्यता और आकांक्षा के पक्ष में मस्तिष्क काम करता चला जाता है और प्रतिपक्षी तर्कों एवं तथ्यों का ध्यान ही नहीं रहता। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी तर्कों को सामने रखा जाना चाहिए। न्यायाधीश को वस्तुस्थिति समझने के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के प्रमाण, साक्षी एवं तर्क सुनने पड़ते हैं। अन्य न्यायाधीशों ने ऐसे प्रसंगों पर क्या-क्या निष्कर्ष निकाले हैं इसका ध्यान रखना पड़ता है। तब कहीं उचित निर्णय करने की स्थिति बनती है। यदि एक ही पक्ष की बात सुनी जाय दूसरा पक्ष कुछ बताये ही नहीं तो स्वभावतः एकांगी निर्णय करने की स्थिति खड़ी हो जायगी। इसमें न्याय के स्थान पर अन्याय का पक्षपात जैसी दुर्घटना घटित हो जायगी। इसमें न्यायाधीश की नीयत का नहीं उस एकांगी परिस्थिति का दोष है जिसमें मन्थन के लिए—काट-छांट के लिए अवसर ही नहीं मिला और न करने योग्य निर्णय कर लिया गया। यही दुर्घटना तब घटित होती है जब एकांगी-एक पक्षीय-विचारों की घुड़दौड़ मस्तिष्क में चलती रहती है और ऐसे निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं जो अनुपयुक्त होने के कारण असफल एवं उपहासास्पद सिद्ध होते हैं।
यदि मन पक्षपाती पूर्वाग्रहों से भरा हो तो फिर आप्त वचन और शास्त्र भी सही मार्गदर्शन कर सकने में असमर्थ रहेंगे। उनकी व्याख्याएं इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर की जाने लगेंगी कि तर्क की दृष्टि से उस प्रतिपादन को चमत्कारी माना जायगा फिर भी शास्त्रकारों और आप्त पुरुषों के मूल मन्तव्य की वास्तविकता के साथ उसकी पटरी बिठाना अति कठिन हो जायगा।
गीतों के अनेकों भाष्य हुए हैं। इन भाष्यकारों ने जो भाष्य किये हैं उनमें उनका अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने का आग्रह ही प्रधान रूप से काम करता है। जान-बूझकर अथवा अनजाने ही वे मूल ग्रन्थकार के वास्तविक उद्देश्य के विपरीत बहुत दूर तक निकल गये हैं। यदि ऐसा न होता तो इतने तरह के परस्पर विरोधी भाष्य एक ही ग्रन्थ के क्योंकर लिखे जा सकते? इनमें से कुछ ही टीकाकार सही हो सकते हैं। कर्त्ता का यह उद्देश्य तो रहा नहीं होगा कि वह ऐसी वस्तु रच दे जिसका तात्पर्य निकालने वाले इस प्रकार के परस्पर विरोधी जंजाल में फंसकर स्वयं भ्रमित हों और दूसरों को भ्रमित करें। रामायण की अनेक चौपाइयों के ऐसे विचित्र अर्थ सुनने में आते हैं जिन्हें यदि मूल रचनाकार के सामने रखा जाय तो स्वयं आश्चर्यचकित होकर रह जायेंगे कि जो बातें कल्पना में भी नहीं थीं वे उनके गले किस प्रकार मढ़ दी गईं।
संसार के मूर्धन्य साहित्यकारों के अपनी कृतियों में भारतीय शास्त्रों और मनीषियों के अनेकों उद्धरण दिये हैं। ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है कि उद्धरणों की शब्द रचना यथावत् है, किन्तु उन्हें इस प्रकार के प्रयोजनों में प्रयुक्त किया गया है जैसा कि उन कथनों का मूल उद्देश्य नहीं था। डी. एच. लारेन्स ने अपनी अन्तःस्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है—‘‘मेरे भीतर एक नहीं कई देवता निवास करते हैं।’’ यहां उनने देवताओं को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह देववाद के मूल प्रतिपादनों के अनुरूप नहीं हैं। हैनरी मिलर की पुस्तकों में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द के उद्धरणों की भरमार है, पर वे मूलतः उन मन्तव्यों के लिए नहीं कहे गये थे जैसा कि मिलर ने सिद्ध किया है। स्टेनबेक ने अपनी पुस्तक ‘केनेरी को’ में संस्कृत कवि विल्हण की कई रचनाओं का उल्लेख किया है। कालिन विल्सन ने मानवी पृथकतावाद के समर्थन में भारत में प्रचलित धर्म दृष्टान्तों का अनेक प्रसंगों में सहारा लिया है। आल्डुआस हक्सले ने प्राचीनता और आधुनिकता के विग्रह में भगवान बुद्ध को आधुनिकता का समर्थक सिद्ध किया है। एरिक फ्राम ने अपनी पुस्तक ‘आर्ट आफ लविंग’ में योरोप में उत्पन्न हुए अनेकों संघर्षों की जड़ अरस्तु के तर्क शास्त्र को बताया है जिसने जनमानस में यह बात बिताई कि संसार में देव और असुर दो ही शक्तियां हैं और दोनों परस्पर विरोधी हैं। यह (ए, एण्ड नान ए) का सिद्धान्त मुद्दतों तक लोगों के दिमागों में गूंजता रहा है और वे यह सोचते रहे कि बुराई पर आक्रमण करके उसे मिटाया जाना चाहिए। अब इसका निर्णय कौन करे कि बुराई किस पक्ष की है? अपनी या पराई? इस निष्कर्ष में फैसला अपने ही पक्ष को सही मानने की ओर झुकता है। हम जो सोचते और करते हैं वही ठीक है। गलती तो अन्य लोग ही कर सकते हैं, वह हमसे क्यों होगी? इसी पूर्वाग्रह से हर व्यक्ति और वर्ग घिरा रहता है। फलतः उसे सामने वाले में ही बुराई दीखती है और उसे मिटाने के लिए तलवार पर धार रखता है। इसी मान्यता ने कलह विद्वेष और आक्रमणों को जन्म दिया है।
उच्चस्तरीय आस्थाओं के प्रति व्यक्ति को निष्ठावान् बनाना अध्यात्मवादी तत्वदर्शन का काम है। धर्म और दर्शन का लक्ष्य यही है। संस्कृति की उपयोगिता इसी में है कि वहमानवी चिन्तन का स्तर ऊंचा उठाये। उसे आत्म गौरव की अनुभूति कराने के साथ-साथ सज्जनता को व्यवहार में उतारने का साहस भी प्रदान करे।
सत्य की उपेक्षा न हो—
आज विज्ञान को अनास्था का सेनापति बनाकर खड़ा कर दिया गया है और उसे विश्रंखित जीवन के सैनिकों की भर्ती करने की छूट दे दी गई है। फलस्वरूप सदाचरण जैसी मानवीय गरिमा आज औंधे मुंह पड़ी सिसक रही है। दूसरी ओर अवांछनीयता उच्छृंखलता का दानव सर्वत्र कबड्डी खेलता घूम रहा है।
अहंकार और व्यामोह का समन्वित रूप बनता है—दुराग्रह। इसमें आवेश और हठ दोनों ही जुड़े रहते हैं। फलतः चिन्तन तन्त्र के लिए यह कठिन पड़ता है कि वह सत्य और तथ्य को ठीक तरह समझ सके और उचित-अनुचित का भेद कर सके। अभ्यस्त मान्यताओं के प्रति एक प्रकार की कट्टरता जुड़ जाती है। इसे अच्छी तरह से सिद्ध करने के लिए परम्पराओं के निर्वाह की दुहाई दी जाती है। उसका समर्थन धर्मशास्त्र, आप्तवचन, देश भक्ति आदि के नाम पर किया जाता है और कई बार तो उसे ईश्वर का आदेश तक घोषित कर दिया जाता है।
अपना धर्म श्रेष्ठ दूसरे का निकृष्ट—अपनी जाति ऊंची दूसरे की नीची—अपनी मान्यता सच दूसरे की झूंठ—ऐसा दुराग्रह यदि आरम्भ से ही हो तो फिर सत्य असत्य का निर्णय हो ही नहीं सकता न्याय और औचित्य की रक्षा के लिए आवश्यक है कि तथ्यों को ढूंढ़ने के लिए खुला मस्तिष्क रखा जाय और अपने पराये का—नये पुराने का—भेदभाव न रखकर विवेक और तर्क का सहारा लेने की नीति अपनाई जाय। सत्य को प्राप्त करने का लक्ष्य इस नीति को अपनाने से पूरा हो सकता है। पक्षपात और दुराग्रह तो सत्य को समझने से इन्कार करना है। ऐसे हठी लोग प्रायः सत्य और सत्यशोधकों को सताने तक में नहीं चूकते।
टेलिस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो ने जब पृथ्वी को गतिशील बताने का सर्वप्रथम साहस किया तो पुरातन पंथी धर्म गुरुओं ने इसे धर्म विरुद्ध ठहराया। उसे तरह-तरह से सताया गया और जेल में बन्द करके सड़ाया गया। सबसे पहले जब पैरिस में रेलगाड़ी चली तो उस प्रचलन का पुरातन पंथियों ने घोर विरोध किया और कहा जो काम हमारे महान पूर्वज नहीं कर सके उन्हें करना अपने पूर्व पुरुषों के गौरव पर बट्टा लगाना है। रेलगाड़ी के चलाने वाले जोसफ केग्नार को उस जुर्म में जेल में डाला गया कि वह ईश्वर के नियमों के विरुद्ध काम करता है। इटली में शरीर शास्त्र की शिक्षा किसी समय अपराध थी। आपरेशन करना पाप समझा जाता था और कोई चिकित्सक छोटा-मोटा आपरेशन भी करता पाया जाता तो उसे मृत्यु दण्ड सुनाया जाता था।
कारीगर रैगर बेकन ने सर्वप्रथम दो कोनों को जोड़कर सूक्ष्म दर्शी यन्त्र बनाया था। इस आविष्कार की निन्दा की गई। उस कारीगर को इस खतरनाक काम को करने के अभियोग में दस वर्ष की कैद सुनाई गई। बेचारा जेल में ही तड़प-तड़प कर मर गया।
रसायन शास्त्र के कुछ नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के अपराध में स्वन्ति अरहीनियस को प्राध्यापक के पद से पदच्युत करके एक छोटा अध्यापक बनाया गया और उसे सनकी ठहराकर अपमानित किया गया। विधि का विधान ही समझिये कि वही सिद्धान्त आगे चलकर विज्ञान जगत में सर्वमान्य हुए और स्वन्ति को उन्हीं पर नोबेल पुरस्कार मिला।
डा. हार्ले ने जब सर्वप्रथम यह कहा कि रक्त नसों में भरा नहीं रहता वरन् चलता रहता है तो समकालीन चिकित्सकों ने उसे खुले आम बेवकूफ कहा। ब्रूनो ने जब अन्य ग्रहों पर भी जीवन होने की सम्भावना बताई तो लोग इतने क्रुद्ध हुए कि उसे जीवित ही जला दिया।
दुराग्रह के अत्याचारों का इतिहास बहुत लम्बा और बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। पिछले दिनों यह हठवादिता बहुत चलती रही है। धर्म परम्परा, देश भक्ति, ईश्वर का आदेश आदि न जाने क्या-क्या नाम इस हठवादिता को दिये जाते हैं। और सत्य एवं धर्म की आत्मा का हनन होता रहा है। मानवी विवेक में निष्पक्ष सत्यशोधक की दृष्टि को ही प्रश्रय मिलना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब धर्म आगे-आगे चले और विज्ञान तथ्यानुयायी बने।