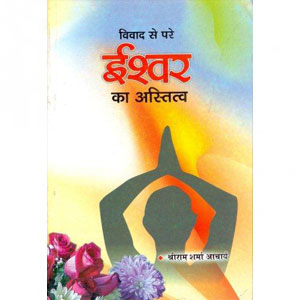विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व 
ईश्वरीय सत्ता के प्रमाण व विधान
Read Scan Version
भगवान् मनु ने कहा है—
मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानसिसृक्षया। —मनु 1।74-75
सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने अपनी इच्छा शक्ति से मन (जीवों) को उत्पन्न किया।
सृष्टि की हलचल की ओर ध्यान जमाकर देखें तो यह सत्य ही प्रतीत होगा कि इच्छाओं के कारण ही लोग या जीव क्रियाशील हैं, यह इच्छायें अनेक भागों में बंटी हुई हैं—(1) दीर्घ-जीवन की इच्छा, (2) कामेच्छा, (3) धन की इच्छा, (4) मान की इच्छा, (5) ज्ञान की इच्छा, (6) न्याय की इच्छा और (7) अमरत्व या आनन्द प्राप्ति की चिर तृप्ति या मोक्ष। इन सात जीवन धाराओं में ही संसार का अविरल प्रवाह चलता चला आ रहा है। इन्हीं की खटपट, दौड़-धूप, ऊहापोह में दुनिया भर की हलचल मची हुई है, इच्छायें न हों तो संसार में कुछ भी न रहे।
इन इच्छाओं की शक्ति से ही सूर्य, अग्नि और आकाश की रचना हुई है। देखने और सुनने में यह बात कुछ अटपटी-सी लगती है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जब हम शोक, क्रोध, काम या प्रेम आदि किसी भी स्थिति में होते हैं तो शारीरिक परमाणुओं में अपनी-अपनी विशेषता वाली गति उत्पन्न होती हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के स्पंदित होते रहते हैं, इससे स्पष्ट है कि शरीर की हलचल इच्छाओं पर आधारित है।
अब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या मूल चेतना में अपने आप इच्छायें व्यक्त करने की शक्ति है। इस बात को वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों से भली प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। जिन्होंने विज्ञान का थोड़ा भी अध्ययन किया होगा, उन्हें ज्ञात होगा कि जड़ पदार्थ (मैटर) को शक्ति (एनर्जी) अथवा विद्युत (इलेक्ट्रिसिटी) में बदल दिया जाता है। इस बात का पता पदार्थ की अति सूक्ष्म अवस्था में पहुंचकर हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। परमाणु भी अन्तिम स्थिति न होकर उनमें भी ‘इलेक्ट्रान’ और ‘प्रोट्रॉन’ आवेश होते हैं। प्रोट्रॉन परमाणु का केन्द्र है और इलेक्ट्रान उस केन्द्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। यह दोनों अंश छोटे-छोटे टुकड़े नहीं हैं वरन् यह धन और ऋण आवेश (इलेक्ट्रिसिटी) है, दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया का नाम ही परमाणु है। इस दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि संसार में जड़ कुछ है ही नहीं। जगत् का मूल तत्त्व विद्युत है और उसी के प्रकम्पन (वाइब्रेशन्स) द्वारा स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों का अनुभव होता है। छोटे-छोटे पौधों, वृक्ष एवं वनस्पति से लेकर पहाड़, समुद्र, पशु-पक्षी, रंग-रूप और अग्नि-वायु, शीत, ग्रीष्म आदि सब विद्युत् चेतना के ही हैं उन्हें देखते हुए भविष्य में और भी बड़े सत्यों का रहस्योद्घाटन होता रहेगा। यह कार्य वैज्ञानिक शोध-पद्धति से ही सम्भव है।
‘सिद्धान्तों, यन्त्रों और आविष्कारों में विज्ञान झांकता भर दिखाई देता है। उन्हें उसकी उपलब्धियां भर कह सकते हैं। वस्तुतः विज्ञान एक जीवन्त प्रवृत्ति है जो सत्य की शोध को अपना लक्ष्य मानती है। भले ही इसके फलस्वरूप पूर्व मान्यताओं पर आंच आती हो अथवा किसी वर्ग विशेष का हित-अनहित होता हो। सत्य को सत्य ही रहना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि में ईश्वर ‘सत्य’ है। उसकी साधना को सत्य की खोज कह सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान को अपने ढंग का ‘आस्तिक’ और उसकी शोध साधना को ईश्वर उपासना कहा जा सकता है।’
आइन्स्टाइन के मतानुसार पदार्थ एवं जीवन का स्वरूप समझना ही नहीं उनका दूरदर्शितापूर्ण सदुपयोग करने का उपाय सोचना भी विज्ञान क्षेत्र में आता है। तत्व-दर्शन को विज्ञान की एक शाखा मानते हैं और जीवन क्षेत्र में रुचि रखने वालों को परामर्श देते हैं— ‘‘जिज्ञासा को जीवन्त रखो और सोचो की तुम क्या कर रहे हो? श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का प्रयत्न करो। बिना दिये पाने का प्रयत्न मत करो। श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन से अथवा व्यक्तियों से जितना लेता है उनसे अनेक गुना उन्हें वापिस करने के प्रयत्न में लगा रहता है।’’
केनोपनिषद् के ऋषि ने परब्रह्म की व्याख्या आइन्स्टाइन से मिलती-जुलती ही की है। उनका प्रतिपादन है—
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं सिद्धि तेदं यदिदमुपासते॥ यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं यदिदमुपासते॥ यच्छोत्रेण न श्रणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं यदिदमुपासते॥ यत्प्राणेन न प्राहिणति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं यदिदमुपासते॥
अर्थात् परब्रह्म ऐसा कोई विचारणीय पदार्थ नहीं जिसे मन द्वारा ग्रहण किया जा सके। वह तो ऐसा तथ्य है जिसके आधार पर मन को मनन शक्ति प्राप्त होती है। उस परम तत्व की सामर्थ्य से ही मन को मनन कर सकने की क्षमता प्राप्त होती है। वह परब्रह्म ही नेत्रों को देखने की, कानों को सुनने की, प्राणों को जीने की शक्ति प्रदान करता है। परब्रह्म ऐसा नहीं है जिसे इन्द्रियों से देखना और मन से समझना सम्भव हो सके। वह सर्वान्तर्यामी और निरपेक्ष है। वह कोई देवता नहीं है और न वैसा है जिसकी परब्रह्म नाम से उपासना की जाती है।
मुण्डकोपनिषद् के ऋषि का अभिमत भी इसी से मिलता-जुलता है। उनका कथन है—
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा- नान्यैर्दैवैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः॥
अर्थात् आंखों से, जीभ से अथवा अन्य इन्द्रियों से उसे जाना नहीं जा सकता। मात्र तप और कर्मकाण्ड भी उसकी अनुभूति नहीं कराते। जिसका मन पवित्र और शान्त है वह निर्मल ज्ञान की सहायता से गम्भीर ध्यान का आश्रय लेकर उसकी प्रतीति कर सकता है।
ज्ञान का अन्तर्ज्ञान के अन्तर एवं कार्य क्षेत्र सम्बन्धी पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में आइन्स्टाइन ने कहा था—‘‘ज्ञान आवश्यक है। उसी के सहारे दैनिक क्रियाकलापों का संचालन और निर्णयों का निर्धारण होता है। फिर भी अन्तर्ज्ञान का अपना क्षेत्र और अस्तित्व है।’’
हमारा मस्तिष्क मात्र वहीं तक सहारा देता है जहां तक कि उसकी जानकारी है अथवा तर्क की उड़ान उड़ती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां चेतना उछल कर किसी ऐसे स्थान पर जा पहुंचती है जहां मस्तिष्क के सहारे पहुंच सकना कठिन है। संसार के महान् आविष्कार इसी रहस्यमयी अन्तःप्रज्ञा के आधार पर सम्भव हुए हैं। वहां से उनको प्रकाश मिला है। प्रमाणित करने वाले अन्वेषण का कार्य तो यह प्रकाश मिलने के उपरान्त आरम्भ होता है।
ज्ञान उपलब्धि के तीन प्रसंग हैं—एक वह जो माता की गोदी से लेकर परिवार एवं सम्पर्क क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर संचित होता है और स्वभाव का अंग बनता है। दूसरा वह जो स्कूली तथा व्यवहार क्षेत्र में अनेकों अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त होता रहता है। तीसरा अन्तिम चरण वह है जिसमें आत्मबोध होता है। जीवन का स्वरूप, उद्देश्य एवं उपयोग मस्तिष्क की जानकारी तक सीमित न रहकर अब आस्था बनकर परिपुष्ट होता है तब उसे आत्मबोध कहते हैं। यह वह उपलब्धि है जिसे पाकर एक सामान्य-सा राजकुमार महान् बुद्ध के रूप में साक्षात् भगवान बन गया था। इस तत्व की छोटी मात्रा भी मनुष्य को अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा और कहीं अधिक सफल बनाती है। ज्ञान भूमिका का यह तीसरा चरण आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वर दर्शन के रूप में माना गया है। आत्मा का एकाकी अस्तित्व आदर्श विहीन और नीरस ही रह जाता है, उसमें सरसता का संचार ईश्वर के समन्वय से ही सम्भव होता है। आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान को एक ही तथ्य का उद्बोधक माना गया है। ईश्वर विश्वास के साथ जुड़ा हुआ आत्म-विश्वास जब विकसित होता है तो उस पर उच्चस्तरीय आदर्शवादिता छाई रहती है। यह आच्छादन सामान्य दृष्टि से भले ही नगण्य-सा प्रतीत होता हो, पर उसका प्रतिफल क्रमशः अधिकाधिक श्रेय, फलदायक, सिद्ध होता चला जाता है।
जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर विश्वास सहायक होता है वह असन्तुलन को सन्तुलन में बदलता है। निराशा के क्षणों में उसकी वह ज्योति चमकती है जिसे दीनबन्धु, भक्त-वत्सल, अशरण–शरण आदि नामों से पुकारते हैं और मातृ तुल्य वात्सल्य प्रदान करने की, आंचल में आश्रय देने की कल्पना करते हैं। सफलताओं के साथ-साथ एक उन्मादी अहंकार जिसमें स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति पनपती है और मर्यादाओं की नीति-नियमों की चिन्ता न करते हुए स्वार्थ साधना एवं अहमन्यता की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने की उच्छृंखलता अपनाता है तो उसे आस्तिकता की भावना ही डराती है। वह कहती है यहां स्वेच्छाचार की किसी को भी छूट नहीं है। सबके ऊपर एक नियामक शक्ति मौजूद है और कर्मफल की दण्ड व्यवस्था भी मौजूद है जो इतनी कठोर है कि मर्यादा तोड़ने वाले को भली प्रकार सबक सिखा सकती है। भगवान की भयानकता से डर कर उच्छृंखलता पर बहुत कुछ नियन्त्रण होता रह सकता है। आस्तिकता में ईश्वर के गुणानवादों का कथन, श्रवण, मनन, चिन्तन जुड़ा हुआ है। ईश्वर सद्गुणों का पुंज है। पवित्रता, करुणा, ममता, दया, उदारता जैसी सद्भावनाएं ईश्वरीय अनुकम्पा के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली विभूतियां हैं। इस मान्यता से ईश्वर सान्निध्य के लिए—उपासना आदि प्रयास करते हुए मनुष्य अधिकाधिक चरित्र-निष्ठ और समाज-निष्ठ बनने का प्रयत्न करता है। समाज-निष्ठा को धार्मिकता और सभ्यता कहते हैं। चरित्र-निष्ठा का दर्शन अध्यात्म कहलाता है उसी का दूसरा नाम संस्कृति भी है। इन्हीं के आधार पर मनुष्य प्रामाणिक और पराक्रमी बनता है। प्रगति के यही दो चरण हैं जिनके सहारे लोग भौतिक एवं आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की मान्यता का प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में सदाशयता और शालीनता की अभिवृद्धि में ही दृष्टिगोचर होता है। यों बुराइयां तो आस्तिकों में भी पाई जाती हैं, पर नास्तिकता अपना लेने पर तो मनुष्य उन मर्यादा उल्लंघन के सम्बन्ध में और भी अधिक निर्भय हो जाता है। सम्भावनाओं की दृष्टि से देखा जाय तो आस्तिक की तुलना में नास्तिक के अनाचार मार्ग पर चल पड़ने की सम्भावना है। श्रेष्ठ मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले के लिए ईश्वर विश्वास एक सुयोग्य एवं सुसम्पन्न साथी की तरह सहायक सिद्ध होता है, वह सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन ही नहीं, वरन् सहायता के आश्वासन भी देता है। इन दिनों आन्तरिक उपलब्धियों के सहारे चलने वाले का साहस प्रतिकूलताओं के बीच भी अविचल बना रहता है। नास्तिक ऐसी किसी सहायता की आशा नहीं करता, साथ ही अपनी दुर्बलताओं एवं कठिनाइयों को देखता रहता है ऐसी दशा में उसे ऐसी अन्तःस्फुरणा का लाभ नहीं मिलता जो अग्रगमन के लिए अनुकूल साधनों से भी अधिक मूल्यवान होती है।
बुद्धि की एक सीमा है। प्रत्येक प्राणी को वह उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मिली है। उसके आधार पर चेतना के परतों को समझना तो दूर पदार्थ के प्रत्यक्ष दर्शन से आगे की—उसकी सूक्ष्म क्षमताओं तक की पूरी जानकारी नहीं हो सकती। प्रकृति के अनेक रहस्यों को जानने में मनुष्य ने आश्चर्यजनक सफलता पाई, पर अभी जो जाना गया है उसकी तुलना में अविज्ञात का विस्तार अधिक है। प्रकृति के नये-नये रहस्यों का उद्घाटन आये दिन होता रहता है। यह क्रम आगे भी चलता रहेगा किन्तु इस भौतिक जगत् की सूक्ष्मतम परिस्थितियों को पूर्णतया जान सकना कभी भी सम्भव न हो सकेगा, क्योंकि प्रकृति के विस्तार की तुलना में मानवी बुद्धि की एक सीमा और मर्यादा है उससे आगे बढ़ सकना उसके लिए सम्भव नहीं है।
इस सन्दर्भ में दार्शनिक विज्ञानवेत्ता हिटक ने अपनी पुस्तक ‘साइन्टिफिक रोमांसेज’ में प्राणियों की बुद्धि सीमाबन्धन के कितने ही उदाहरण दिये हैं। वे आंख से न दीख सकने वाले एक जीव ‘माइक्रोव’ का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उसे केवल लम्बाई-चौड़ाई की दो दिशाओं का ही ज्ञान है। ऊंचाई से वह परिचित नहीं है। उसे समतल फर्श पर रखा जाय तो वह चलता ही रहेगा किन्तु यदि आगे कोई तख्ती खड़ी कर दी जाय तो रुक भर जायेगा उसका कारण न समझ सकेगा और न उससे बच निकलने का कोई उपाय ही करेगा। यदि तख्ती हटा दी जाय तो फिर चलने लगेगा किन्तु उस अवरोध के खड़े होने या हटने से उसकी गति पर क्यों प्रभाव पड़ा इसका कुछ भी कारण न समझ सकेगा। तख्ती खड़ी होने या हटने के क्रिया-कलाप के सम्बन्ध में कोई कल्पना तक कर सकना उसके लिए सम्भव न होगा। इतने पर भी माइक्रोव के अतिरिक्त अन्य प्राणी यह तो स्वीकार नहीं ही करेंगे कि ऊंचाई का कोई आयाम ही नहीं होता। लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई के तीन आयाम सर्वविदित हैं। चौथा आयाम बुद्धि का भी है। बुद्धि की भी एक सीमा मर्यादा है। वह न तो असीम है- न निभ्रान्त और न सर्वज्ञ है। हर प्राणी की आवश्यकता को देखते हुए प्रकृति ने उसे कामचलाऊ मात्रा में उस उपहार से सुसज्जित किया है। उसमें घट-बढ़ भी एक सीमित मात्रा में ही हो सकती है। मानसिक अपंगों की बात दूसरी है।
कर्मफल न चाहते हुए भी मिलते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसे अशुभ कर्मों के फलस्वरूप दण्ड मिले। कोई नहीं चाहता कि पुरुषार्थ के अनुपात में ही सफलता मिले। हर कोई दुःख से बचना और सुख का अधिकाधिक लाभ पाना चाहता है। पर यह इच्छा कहां पूरी होती है? नियामक शक्ति द्वारा पदार्थों की तरह ही प्राणियों पर भी अंकुश रखा जाता है और जहां भी वे आलस्य प्रमाद बरतते हैं वहीं असफलताओं की, पिछड़ेपन की हानि उठाते हैं। व्यवस्था तोड़ते ही ठोकर खाते और दण्ड पाते हैं। विष खाना और पानी में कूदना अपने हाथ की बात है, पर उसके दुष्परिणामों से बच सकना कभी-कभी संयोगवश ही होता है। अपनी ही चेतना की सूक्ष्म परतों में ऐसी व्यवस्था ‘फिट’ है कि वह कुविचारों, कुकर्मों का प्रतिफल स्वसंचालित पद्धति से अपने आप ही प्रस्तुत करती रहती है। इसे झुठलाना या इससे बच निकालना भी किसी के हाथ में नहीं। देर तो होती है, पर अन्धेर की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। आज के कर्मों का फल कल मिले इसमें देरी तो हो सकती है किन्तु कुछ भी करते रहने और मनचाहे प्रतिफल पाने की छूट किसी को भी नहीं है। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की प्रक्रिया से सभी को असुविधा, अनुभव होती है। सभी सुविधाजनक स्थिति में स्थिर रहना चाहते हैं, पर सृष्टि क्रम के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। इस व्यवस्था प्रवाह को ईश्वर समझा जा सकता है।
अन्तःकरण में एक ऐसी शक्ति काम करती है जो सन्मार्ग पर चलने से प्रसन्न, सन्तुष्ट हुई दिखाई पड़ती है और कुपंथ अपनाने पर खिन्नता, उद्विग्नता का अनुभव करती है। अन्तरात्मा की इसी परत में ईश्वर झांकता हुआ देखा जा सकता है।
मानव जीवन में समता, सहयोग, शिक्षा, साहस, चरित्र और सुरक्षा जैसे उच्चस्तरीय तत्वों के अभिवर्धन की आवश्यकता है। यह मनन स्थितियां भी हैं परिस्थितियां भी। इन्हें आस्थाओं की गहराई में प्रवेश करने के लिए जिस दर्शन की आवश्यकता है वह आस्तिकता का ही हो सकता है। निजी और तात्कालिक संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाकर ही सामाजिक और आदर्शवादी मूल्यों का परिपोषण हो सकता है। प्रत्यक्षवाद का दबाव यह रहता है कि अपना सामयिक स्वार्थ सिद्ध किया जाय भले ही उसके फलस्वरूप भविष्य में अपने को हानि उठानी पड़े अथवा सार्वजनिक अहित करना पड़े। इस पशु प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने से ही मानवी आदर्शों की नींव रखी जा सकती है। इस स्तर की आस्थाएं उत्पन्न करने में आस्तिकतावादी दर्शन से बढ़कर और कोई मनोवैज्ञानिक स्थापना हो नहीं सकेगी। देश-भक्ति, समाजनिष्ठा, अति मानव आदि के कितने ही विकल्प इसके लिए रखे गये और प्रयुक्त होते रहे हैं, पर उनसे बौद्धिकता अधिक और आध्यात्मिकता स्वल्प रहने से आस्था न बन की और नीति के रूप में जो जाना माना गया था वह संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्ति के सामने ठहर न सका। मानव जीवन की गरिमा और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आस्थाओं की। आस्तिकता का मूलभूत आधार इसी स्तर की आस्थाएं उत्पन्न करना है।
ईश्वर का प्रेम किनके लिए?
आस्तिकता के इस मूलभूत आधार को जिन्होंने अपनी जीवन शैली बनाया उनके जीवन व क्रियाकलापों को परमार्थ निष्ठा का आदर्श कहा जा सकता है। परमार्थ का अर्थ ही यह है कि जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन की पूर्ति होती हो। इसी कारण परमार्थ परायणता को आस्तिकता का आधार दर्शन कहा जा सकता है।
परमार्थ बुद्धि से जो कुछ भी किया जाता है, जिस किसी के लिए भी किया जाता है वह लौटकर उस करने वाले के पास ही पहुंचता है। तुम्हारी यह आकांक्षा वस्तुतः अपने आपको प्यार करने, श्रेष्ठ मानने और आत्मा के सामने आत्म समर्पण करने के रूप में ही विकसित होगी। दर्पण में सुन्दर छवि देखने की प्रसन्नता- वस्तुतः अपनी ही सुसज्जा की अभिव्यक्ति है। दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना उसी के लिए सम्भव है जो भीतर से श्रेष्ठ है। प्रभु की राह पर बढ़ाया गया हर कदम औरों के लिए किया जाता है वस्तुतः वह अपने लिए किया हुआ कर्म ही है। दूसरों के लिए अन्याय करना अपने साथ ही अन्याय करना है। हम अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं ठग सकते। दूसरों के प्रति असज्जनता बरत कर अपने आपके साथ ही दुष्ट दुर्व्यवहार किया जाता है।
दूसरों को प्रसन्न करना अपने आप को प्रसन्न करने का ही क्रिया-कलाप है। गेंद को उछालना अपनी मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाने के अतिरिक्त और क्या है। गेंद को उछालकर हम उस पर कोई एहसान नहीं करते। इसके बिना उसका कुछ हर्ज नहीं होगा। यदि खेलना बन्द कर दिया जाय तो उन क्रीड़ा उपकरणों की क्या क्षति हो सकती है? अपने को ही बलिष्ठता के आनन्द से वंचित रहना पड़ेगा।
ईश्वर रूठा हुआ नहीं है कि से मनाने की मनुहार करनी पड़े। रूठा तो अपना स्वभाव और कर्म है। मानना उसी को चाहिए, अपने आप से ही प्रार्थना करें कि कुचाल छोड़ें। मन को मना लिया— उसकी प्रसन्नता के लिए ही किये जा रहे हैं। दूसरों की सेवा, सहायता अपनी ही सेवा सहायता है।
प्रार्थना उसी की सार्थक है जो आत्मा को परमात्मा में घुला देने के लिए व्याकुल लिए हुए हो। जो अपने को परमात्मा जैसा महान बनाने के लिए तड़पता है— जो प्रभु को जीवन के कण-कण में घुला लेने के लिए बेचैन है। जो किसी का होकर जीना चाहता है उसी को भक्त कहना चाहिए। दूसरे तो विदूषक हैं। लेने के लिए किया हुआ भजन वस्तुतः प्रभु प्रेम का निर्गम उपहास है भक्ति में तो आत्म समर्पण के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। वहां देने की ही बात सूझती है लेने की इच्छा ही कहां रहती है। ईश्वर का विश्वास, सत्कर्मों की कसौटी पर ही परखा जा सकता है। जो भगवान पर भरोसा करेगा वह उसके विधान और निर्देश को भी अंगीकार करेगा। भक्ति और अवज्ञा का ताल-मेल बैठता कहां है?
हम अपने आपको प्यार करें, ताकि ईश्वर से प्यार कर सकने योग्य बन सकें। हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करें ताकि ईश्वर के निकट बैठ सकने की पात्रता प्राप्त कर सकें। जिसने अपने अन्तःकरण को प्यार से ओत-प्रोत कर लिया, जिसके चिन्तन और कर्तृत्व में प्यार बिखरा पड़ता है ईश्वर का प्यार केवल उसी को मिलेगा, जो दीपक की तरह जल कर प्रकाश उत्पन्न करने को तैयार है, प्रभु की ज्योति का अवतरण उसी पर होगा। ईश्वर का अस्तित्व विवाद का नहीं अनुभव का विषय है। जो उस अस्तित्व का जितना अधिक अनुभव करेगा, उतना ही प्रकाशपूर्ण उसका जीवन होता जायगा।
मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानसिसृक्षया। —मनु 1।74-75
सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने अपनी इच्छा शक्ति से मन (जीवों) को उत्पन्न किया।
सृष्टि की हलचल की ओर ध्यान जमाकर देखें तो यह सत्य ही प्रतीत होगा कि इच्छाओं के कारण ही लोग या जीव क्रियाशील हैं, यह इच्छायें अनेक भागों में बंटी हुई हैं—(1) दीर्घ-जीवन की इच्छा, (2) कामेच्छा, (3) धन की इच्छा, (4) मान की इच्छा, (5) ज्ञान की इच्छा, (6) न्याय की इच्छा और (7) अमरत्व या आनन्द प्राप्ति की चिर तृप्ति या मोक्ष। इन सात जीवन धाराओं में ही संसार का अविरल प्रवाह चलता चला आ रहा है। इन्हीं की खटपट, दौड़-धूप, ऊहापोह में दुनिया भर की हलचल मची हुई है, इच्छायें न हों तो संसार में कुछ भी न रहे।
इन इच्छाओं की शक्ति से ही सूर्य, अग्नि और आकाश की रचना हुई है। देखने और सुनने में यह बात कुछ अटपटी-सी लगती है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जब हम शोक, क्रोध, काम या प्रेम आदि किसी भी स्थिति में होते हैं तो शारीरिक परमाणुओं में अपनी-अपनी विशेषता वाली गति उत्पन्न होती हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के स्पंदित होते रहते हैं, इससे स्पष्ट है कि शरीर की हलचल इच्छाओं पर आधारित है।
अब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या मूल चेतना में अपने आप इच्छायें व्यक्त करने की शक्ति है। इस बात को वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों से भली प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। जिन्होंने विज्ञान का थोड़ा भी अध्ययन किया होगा, उन्हें ज्ञात होगा कि जड़ पदार्थ (मैटर) को शक्ति (एनर्जी) अथवा विद्युत (इलेक्ट्रिसिटी) में बदल दिया जाता है। इस बात का पता पदार्थ की अति सूक्ष्म अवस्था में पहुंचकर हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। परमाणु भी अन्तिम स्थिति न होकर उनमें भी ‘इलेक्ट्रान’ और ‘प्रोट्रॉन’ आवेश होते हैं। प्रोट्रॉन परमाणु का केन्द्र है और इलेक्ट्रान उस केन्द्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। यह दोनों अंश छोटे-छोटे टुकड़े नहीं हैं वरन् यह धन और ऋण आवेश (इलेक्ट्रिसिटी) है, दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया का नाम ही परमाणु है। इस दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि संसार में जड़ कुछ है ही नहीं। जगत् का मूल तत्त्व विद्युत है और उसी के प्रकम्पन (वाइब्रेशन्स) द्वारा स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों का अनुभव होता है। छोटे-छोटे पौधों, वृक्ष एवं वनस्पति से लेकर पहाड़, समुद्र, पशु-पक्षी, रंग-रूप और अग्नि-वायु, शीत, ग्रीष्म आदि सब विद्युत् चेतना के ही हैं उन्हें देखते हुए भविष्य में और भी बड़े सत्यों का रहस्योद्घाटन होता रहेगा। यह कार्य वैज्ञानिक शोध-पद्धति से ही सम्भव है।
‘सिद्धान्तों, यन्त्रों और आविष्कारों में विज्ञान झांकता भर दिखाई देता है। उन्हें उसकी उपलब्धियां भर कह सकते हैं। वस्तुतः विज्ञान एक जीवन्त प्रवृत्ति है जो सत्य की शोध को अपना लक्ष्य मानती है। भले ही इसके फलस्वरूप पूर्व मान्यताओं पर आंच आती हो अथवा किसी वर्ग विशेष का हित-अनहित होता हो। सत्य को सत्य ही रहना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि में ईश्वर ‘सत्य’ है। उसकी साधना को सत्य की खोज कह सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान को अपने ढंग का ‘आस्तिक’ और उसकी शोध साधना को ईश्वर उपासना कहा जा सकता है।’
आइन्स्टाइन के मतानुसार पदार्थ एवं जीवन का स्वरूप समझना ही नहीं उनका दूरदर्शितापूर्ण सदुपयोग करने का उपाय सोचना भी विज्ञान क्षेत्र में आता है। तत्व-दर्शन को विज्ञान की एक शाखा मानते हैं और जीवन क्षेत्र में रुचि रखने वालों को परामर्श देते हैं— ‘‘जिज्ञासा को जीवन्त रखो और सोचो की तुम क्या कर रहे हो? श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का प्रयत्न करो। बिना दिये पाने का प्रयत्न मत करो। श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन से अथवा व्यक्तियों से जितना लेता है उनसे अनेक गुना उन्हें वापिस करने के प्रयत्न में लगा रहता है।’’
केनोपनिषद् के ऋषि ने परब्रह्म की व्याख्या आइन्स्टाइन से मिलती-जुलती ही की है। उनका प्रतिपादन है—
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं सिद्धि तेदं यदिदमुपासते॥ यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं यदिदमुपासते॥ यच्छोत्रेण न श्रणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं यदिदमुपासते॥ यत्प्राणेन न प्राहिणति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं यदिदमुपासते॥
अर्थात् परब्रह्म ऐसा कोई विचारणीय पदार्थ नहीं जिसे मन द्वारा ग्रहण किया जा सके। वह तो ऐसा तथ्य है जिसके आधार पर मन को मनन शक्ति प्राप्त होती है। उस परम तत्व की सामर्थ्य से ही मन को मनन कर सकने की क्षमता प्राप्त होती है। वह परब्रह्म ही नेत्रों को देखने की, कानों को सुनने की, प्राणों को जीने की शक्ति प्रदान करता है। परब्रह्म ऐसा नहीं है जिसे इन्द्रियों से देखना और मन से समझना सम्भव हो सके। वह सर्वान्तर्यामी और निरपेक्ष है। वह कोई देवता नहीं है और न वैसा है जिसकी परब्रह्म नाम से उपासना की जाती है।
मुण्डकोपनिषद् के ऋषि का अभिमत भी इसी से मिलता-जुलता है। उनका कथन है—
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा- नान्यैर्दैवैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः॥
अर्थात् आंखों से, जीभ से अथवा अन्य इन्द्रियों से उसे जाना नहीं जा सकता। मात्र तप और कर्मकाण्ड भी उसकी अनुभूति नहीं कराते। जिसका मन पवित्र और शान्त है वह निर्मल ज्ञान की सहायता से गम्भीर ध्यान का आश्रय लेकर उसकी प्रतीति कर सकता है।
ज्ञान का अन्तर्ज्ञान के अन्तर एवं कार्य क्षेत्र सम्बन्धी पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में आइन्स्टाइन ने कहा था—‘‘ज्ञान आवश्यक है। उसी के सहारे दैनिक क्रियाकलापों का संचालन और निर्णयों का निर्धारण होता है। फिर भी अन्तर्ज्ञान का अपना क्षेत्र और अस्तित्व है।’’
हमारा मस्तिष्क मात्र वहीं तक सहारा देता है जहां तक कि उसकी जानकारी है अथवा तर्क की उड़ान उड़ती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां चेतना उछल कर किसी ऐसे स्थान पर जा पहुंचती है जहां मस्तिष्क के सहारे पहुंच सकना कठिन है। संसार के महान् आविष्कार इसी रहस्यमयी अन्तःप्रज्ञा के आधार पर सम्भव हुए हैं। वहां से उनको प्रकाश मिला है। प्रमाणित करने वाले अन्वेषण का कार्य तो यह प्रकाश मिलने के उपरान्त आरम्भ होता है।
ज्ञान उपलब्धि के तीन प्रसंग हैं—एक वह जो माता की गोदी से लेकर परिवार एवं सम्पर्क क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर संचित होता है और स्वभाव का अंग बनता है। दूसरा वह जो स्कूली तथा व्यवहार क्षेत्र में अनेकों अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त होता रहता है। तीसरा अन्तिम चरण वह है जिसमें आत्मबोध होता है। जीवन का स्वरूप, उद्देश्य एवं उपयोग मस्तिष्क की जानकारी तक सीमित न रहकर अब आस्था बनकर परिपुष्ट होता है तब उसे आत्मबोध कहते हैं। यह वह उपलब्धि है जिसे पाकर एक सामान्य-सा राजकुमार महान् बुद्ध के रूप में साक्षात् भगवान बन गया था। इस तत्व की छोटी मात्रा भी मनुष्य को अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा और कहीं अधिक सफल बनाती है। ज्ञान भूमिका का यह तीसरा चरण आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वर दर्शन के रूप में माना गया है। आत्मा का एकाकी अस्तित्व आदर्श विहीन और नीरस ही रह जाता है, उसमें सरसता का संचार ईश्वर के समन्वय से ही सम्भव होता है। आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान को एक ही तथ्य का उद्बोधक माना गया है। ईश्वर विश्वास के साथ जुड़ा हुआ आत्म-विश्वास जब विकसित होता है तो उस पर उच्चस्तरीय आदर्शवादिता छाई रहती है। यह आच्छादन सामान्य दृष्टि से भले ही नगण्य-सा प्रतीत होता हो, पर उसका प्रतिफल क्रमशः अधिकाधिक श्रेय, फलदायक, सिद्ध होता चला जाता है।
जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर विश्वास सहायक होता है वह असन्तुलन को सन्तुलन में बदलता है। निराशा के क्षणों में उसकी वह ज्योति चमकती है जिसे दीनबन्धु, भक्त-वत्सल, अशरण–शरण आदि नामों से पुकारते हैं और मातृ तुल्य वात्सल्य प्रदान करने की, आंचल में आश्रय देने की कल्पना करते हैं। सफलताओं के साथ-साथ एक उन्मादी अहंकार जिसमें स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति पनपती है और मर्यादाओं की नीति-नियमों की चिन्ता न करते हुए स्वार्थ साधना एवं अहमन्यता की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने की उच्छृंखलता अपनाता है तो उसे आस्तिकता की भावना ही डराती है। वह कहती है यहां स्वेच्छाचार की किसी को भी छूट नहीं है। सबके ऊपर एक नियामक शक्ति मौजूद है और कर्मफल की दण्ड व्यवस्था भी मौजूद है जो इतनी कठोर है कि मर्यादा तोड़ने वाले को भली प्रकार सबक सिखा सकती है। भगवान की भयानकता से डर कर उच्छृंखलता पर बहुत कुछ नियन्त्रण होता रह सकता है। आस्तिकता में ईश्वर के गुणानवादों का कथन, श्रवण, मनन, चिन्तन जुड़ा हुआ है। ईश्वर सद्गुणों का पुंज है। पवित्रता, करुणा, ममता, दया, उदारता जैसी सद्भावनाएं ईश्वरीय अनुकम्पा के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली विभूतियां हैं। इस मान्यता से ईश्वर सान्निध्य के लिए—उपासना आदि प्रयास करते हुए मनुष्य अधिकाधिक चरित्र-निष्ठ और समाज-निष्ठ बनने का प्रयत्न करता है। समाज-निष्ठा को धार्मिकता और सभ्यता कहते हैं। चरित्र-निष्ठा का दर्शन अध्यात्म कहलाता है उसी का दूसरा नाम संस्कृति भी है। इन्हीं के आधार पर मनुष्य प्रामाणिक और पराक्रमी बनता है। प्रगति के यही दो चरण हैं जिनके सहारे लोग भौतिक एवं आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की मान्यता का प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में सदाशयता और शालीनता की अभिवृद्धि में ही दृष्टिगोचर होता है। यों बुराइयां तो आस्तिकों में भी पाई जाती हैं, पर नास्तिकता अपना लेने पर तो मनुष्य उन मर्यादा उल्लंघन के सम्बन्ध में और भी अधिक निर्भय हो जाता है। सम्भावनाओं की दृष्टि से देखा जाय तो आस्तिक की तुलना में नास्तिक के अनाचार मार्ग पर चल पड़ने की सम्भावना है। श्रेष्ठ मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले के लिए ईश्वर विश्वास एक सुयोग्य एवं सुसम्पन्न साथी की तरह सहायक सिद्ध होता है, वह सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन ही नहीं, वरन् सहायता के आश्वासन भी देता है। इन दिनों आन्तरिक उपलब्धियों के सहारे चलने वाले का साहस प्रतिकूलताओं के बीच भी अविचल बना रहता है। नास्तिक ऐसी किसी सहायता की आशा नहीं करता, साथ ही अपनी दुर्बलताओं एवं कठिनाइयों को देखता रहता है ऐसी दशा में उसे ऐसी अन्तःस्फुरणा का लाभ नहीं मिलता जो अग्रगमन के लिए अनुकूल साधनों से भी अधिक मूल्यवान होती है।
बुद्धि की एक सीमा है। प्रत्येक प्राणी को वह उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मिली है। उसके आधार पर चेतना के परतों को समझना तो दूर पदार्थ के प्रत्यक्ष दर्शन से आगे की—उसकी सूक्ष्म क्षमताओं तक की पूरी जानकारी नहीं हो सकती। प्रकृति के अनेक रहस्यों को जानने में मनुष्य ने आश्चर्यजनक सफलता पाई, पर अभी जो जाना गया है उसकी तुलना में अविज्ञात का विस्तार अधिक है। प्रकृति के नये-नये रहस्यों का उद्घाटन आये दिन होता रहता है। यह क्रम आगे भी चलता रहेगा किन्तु इस भौतिक जगत् की सूक्ष्मतम परिस्थितियों को पूर्णतया जान सकना कभी भी सम्भव न हो सकेगा, क्योंकि प्रकृति के विस्तार की तुलना में मानवी बुद्धि की एक सीमा और मर्यादा है उससे आगे बढ़ सकना उसके लिए सम्भव नहीं है।
इस सन्दर्भ में दार्शनिक विज्ञानवेत्ता हिटक ने अपनी पुस्तक ‘साइन्टिफिक रोमांसेज’ में प्राणियों की बुद्धि सीमाबन्धन के कितने ही उदाहरण दिये हैं। वे आंख से न दीख सकने वाले एक जीव ‘माइक्रोव’ का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उसे केवल लम्बाई-चौड़ाई की दो दिशाओं का ही ज्ञान है। ऊंचाई से वह परिचित नहीं है। उसे समतल फर्श पर रखा जाय तो वह चलता ही रहेगा किन्तु यदि आगे कोई तख्ती खड़ी कर दी जाय तो रुक भर जायेगा उसका कारण न समझ सकेगा और न उससे बच निकलने का कोई उपाय ही करेगा। यदि तख्ती हटा दी जाय तो फिर चलने लगेगा किन्तु उस अवरोध के खड़े होने या हटने से उसकी गति पर क्यों प्रभाव पड़ा इसका कुछ भी कारण न समझ सकेगा। तख्ती खड़ी होने या हटने के क्रिया-कलाप के सम्बन्ध में कोई कल्पना तक कर सकना उसके लिए सम्भव न होगा। इतने पर भी माइक्रोव के अतिरिक्त अन्य प्राणी यह तो स्वीकार नहीं ही करेंगे कि ऊंचाई का कोई आयाम ही नहीं होता। लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई के तीन आयाम सर्वविदित हैं। चौथा आयाम बुद्धि का भी है। बुद्धि की भी एक सीमा मर्यादा है। वह न तो असीम है- न निभ्रान्त और न सर्वज्ञ है। हर प्राणी की आवश्यकता को देखते हुए प्रकृति ने उसे कामचलाऊ मात्रा में उस उपहार से सुसज्जित किया है। उसमें घट-बढ़ भी एक सीमित मात्रा में ही हो सकती है। मानसिक अपंगों की बात दूसरी है।
कर्मफल न चाहते हुए भी मिलते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसे अशुभ कर्मों के फलस्वरूप दण्ड मिले। कोई नहीं चाहता कि पुरुषार्थ के अनुपात में ही सफलता मिले। हर कोई दुःख से बचना और सुख का अधिकाधिक लाभ पाना चाहता है। पर यह इच्छा कहां पूरी होती है? नियामक शक्ति द्वारा पदार्थों की तरह ही प्राणियों पर भी अंकुश रखा जाता है और जहां भी वे आलस्य प्रमाद बरतते हैं वहीं असफलताओं की, पिछड़ेपन की हानि उठाते हैं। व्यवस्था तोड़ते ही ठोकर खाते और दण्ड पाते हैं। विष खाना और पानी में कूदना अपने हाथ की बात है, पर उसके दुष्परिणामों से बच सकना कभी-कभी संयोगवश ही होता है। अपनी ही चेतना की सूक्ष्म परतों में ऐसी व्यवस्था ‘फिट’ है कि वह कुविचारों, कुकर्मों का प्रतिफल स्वसंचालित पद्धति से अपने आप ही प्रस्तुत करती रहती है। इसे झुठलाना या इससे बच निकालना भी किसी के हाथ में नहीं। देर तो होती है, पर अन्धेर की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। आज के कर्मों का फल कल मिले इसमें देरी तो हो सकती है किन्तु कुछ भी करते रहने और मनचाहे प्रतिफल पाने की छूट किसी को भी नहीं है। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की प्रक्रिया से सभी को असुविधा, अनुभव होती है। सभी सुविधाजनक स्थिति में स्थिर रहना चाहते हैं, पर सृष्टि क्रम के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। इस व्यवस्था प्रवाह को ईश्वर समझा जा सकता है।
अन्तःकरण में एक ऐसी शक्ति काम करती है जो सन्मार्ग पर चलने से प्रसन्न, सन्तुष्ट हुई दिखाई पड़ती है और कुपंथ अपनाने पर खिन्नता, उद्विग्नता का अनुभव करती है। अन्तरात्मा की इसी परत में ईश्वर झांकता हुआ देखा जा सकता है।
मानव जीवन में समता, सहयोग, शिक्षा, साहस, चरित्र और सुरक्षा जैसे उच्चस्तरीय तत्वों के अभिवर्धन की आवश्यकता है। यह मनन स्थितियां भी हैं परिस्थितियां भी। इन्हें आस्थाओं की गहराई में प्रवेश करने के लिए जिस दर्शन की आवश्यकता है वह आस्तिकता का ही हो सकता है। निजी और तात्कालिक संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाकर ही सामाजिक और आदर्शवादी मूल्यों का परिपोषण हो सकता है। प्रत्यक्षवाद का दबाव यह रहता है कि अपना सामयिक स्वार्थ सिद्ध किया जाय भले ही उसके फलस्वरूप भविष्य में अपने को हानि उठानी पड़े अथवा सार्वजनिक अहित करना पड़े। इस पशु प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने से ही मानवी आदर्शों की नींव रखी जा सकती है। इस स्तर की आस्थाएं उत्पन्न करने में आस्तिकतावादी दर्शन से बढ़कर और कोई मनोवैज्ञानिक स्थापना हो नहीं सकेगी। देश-भक्ति, समाजनिष्ठा, अति मानव आदि के कितने ही विकल्प इसके लिए रखे गये और प्रयुक्त होते रहे हैं, पर उनसे बौद्धिकता अधिक और आध्यात्मिकता स्वल्प रहने से आस्था न बन की और नीति के रूप में जो जाना माना गया था वह संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्ति के सामने ठहर न सका। मानव जीवन की गरिमा और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आस्थाओं की। आस्तिकता का मूलभूत आधार इसी स्तर की आस्थाएं उत्पन्न करना है।
ईश्वर का प्रेम किनके लिए?
आस्तिकता के इस मूलभूत आधार को जिन्होंने अपनी जीवन शैली बनाया उनके जीवन व क्रियाकलापों को परमार्थ निष्ठा का आदर्श कहा जा सकता है। परमार्थ का अर्थ ही यह है कि जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन की पूर्ति होती हो। इसी कारण परमार्थ परायणता को आस्तिकता का आधार दर्शन कहा जा सकता है।
परमार्थ बुद्धि से जो कुछ भी किया जाता है, जिस किसी के लिए भी किया जाता है वह लौटकर उस करने वाले के पास ही पहुंचता है। तुम्हारी यह आकांक्षा वस्तुतः अपने आपको प्यार करने, श्रेष्ठ मानने और आत्मा के सामने आत्म समर्पण करने के रूप में ही विकसित होगी। दर्पण में सुन्दर छवि देखने की प्रसन्नता- वस्तुतः अपनी ही सुसज्जा की अभिव्यक्ति है। दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना उसी के लिए सम्भव है जो भीतर से श्रेष्ठ है। प्रभु की राह पर बढ़ाया गया हर कदम औरों के लिए किया जाता है वस्तुतः वह अपने लिए किया हुआ कर्म ही है। दूसरों के लिए अन्याय करना अपने साथ ही अन्याय करना है। हम अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं ठग सकते। दूसरों के प्रति असज्जनता बरत कर अपने आपके साथ ही दुष्ट दुर्व्यवहार किया जाता है।
दूसरों को प्रसन्न करना अपने आप को प्रसन्न करने का ही क्रिया-कलाप है। गेंद को उछालना अपनी मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाने के अतिरिक्त और क्या है। गेंद को उछालकर हम उस पर कोई एहसान नहीं करते। इसके बिना उसका कुछ हर्ज नहीं होगा। यदि खेलना बन्द कर दिया जाय तो उन क्रीड़ा उपकरणों की क्या क्षति हो सकती है? अपने को ही बलिष्ठता के आनन्द से वंचित रहना पड़ेगा।
ईश्वर रूठा हुआ नहीं है कि से मनाने की मनुहार करनी पड़े। रूठा तो अपना स्वभाव और कर्म है। मानना उसी को चाहिए, अपने आप से ही प्रार्थना करें कि कुचाल छोड़ें। मन को मना लिया— उसकी प्रसन्नता के लिए ही किये जा रहे हैं। दूसरों की सेवा, सहायता अपनी ही सेवा सहायता है।
प्रार्थना उसी की सार्थक है जो आत्मा को परमात्मा में घुला देने के लिए व्याकुल लिए हुए हो। जो अपने को परमात्मा जैसा महान बनाने के लिए तड़पता है— जो प्रभु को जीवन के कण-कण में घुला लेने के लिए बेचैन है। जो किसी का होकर जीना चाहता है उसी को भक्त कहना चाहिए। दूसरे तो विदूषक हैं। लेने के लिए किया हुआ भजन वस्तुतः प्रभु प्रेम का निर्गम उपहास है भक्ति में तो आत्म समर्पण के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। वहां देने की ही बात सूझती है लेने की इच्छा ही कहां रहती है। ईश्वर का विश्वास, सत्कर्मों की कसौटी पर ही परखा जा सकता है। जो भगवान पर भरोसा करेगा वह उसके विधान और निर्देश को भी अंगीकार करेगा। भक्ति और अवज्ञा का ताल-मेल बैठता कहां है?
हम अपने आपको प्यार करें, ताकि ईश्वर से प्यार कर सकने योग्य बन सकें। हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करें ताकि ईश्वर के निकट बैठ सकने की पात्रता प्राप्त कर सकें। जिसने अपने अन्तःकरण को प्यार से ओत-प्रोत कर लिया, जिसके चिन्तन और कर्तृत्व में प्यार बिखरा पड़ता है ईश्वर का प्यार केवल उसी को मिलेगा, जो दीपक की तरह जल कर प्रकाश उत्पन्न करने को तैयार है, प्रभु की ज्योति का अवतरण उसी पर होगा। ईश्वर का अस्तित्व विवाद का नहीं अनुभव का विषय है। जो उस अस्तित्व का जितना अधिक अनुभव करेगा, उतना ही प्रकाशपूर्ण उसका जीवन होता जायगा।