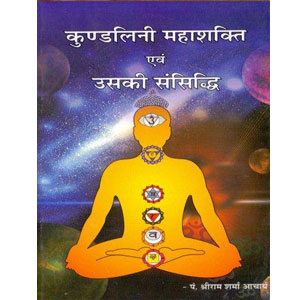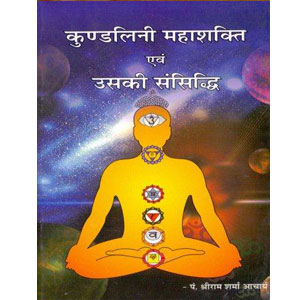कुण्डलिनी महाशक्ति और उसकी संसिद्धि 
कुण्डलिनी साधना स्वरूप और उद्देश्य
Read Scan Versionमस्तिष्क की तीक्ष्णता, बौद्धिक प्रखरता के माध्यम से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों से सभी परिचित हैं बुद्धिमान और सुशिक्षित व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही लोग शिक्षा साधना में मुक्त हस्त से धन और समय लगाते हैं। भारतीय ऋषियों और योगियों ने इस प्रखरता, तेजस्विता का केन्द्र ब्रह्मरन्ध्र बताया है। उसे मस्तिष्क का नाभिक-न्यूक्लियस भी कहा जा सकता है। इसके सहारे न केवल मस्तिष्क का स्तर ‘प्रभावित होता है वरन् सूक्ष्म जगत के साथ भी वैसे ही आदान प्रदान का द्वार खुलता है जैसा कि पृथ्वी का सूर्य एवं अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों के साथ चलता है।
मानवी काया की धुरी ब्रह्मरंध्र स्थित सहस्रार चक्र को बताया जाता है। यह केन्द्र न केवल अपने क्षेत्र मस्तिष्क को प्रभावित करता है वरन् उसके स्तर का भी निर्धारण करता है साथ ही ब्रह्मांडीय चेतना के साथ सम्पर्क बना कर आदान प्रदान का पथ प्रशस्त करता है। भौतिक ऋद्धियां और आत्मिक सिद्धियां जागृत सहस्रार के सहारे निखिल ब्रह्मांड से आकर्षित की जा सकती है। वृक्ष अपने चुम्बकत्व से वर्षा को आकर्षित करते हैं। धातु खदानें अपने चुम्बकत्व से सजातीय धातु कणों को खींचती और जमा करती रहती हैं। सहस्रार में जैसा भी चुम्बकत्व हो उसी स्तर का अदृश्य विश्व वैभव खिंचता और एकत्रित होता रहता है। यही जीवन का अदृश्य उपार्जन उसके स्तर तथा व्यक्तित्व के स्वरूप की पूंजी सम्पत्ति बनती तथा उसके व्यक्तित्व का नियमन निर्धारण करती है। चेतन और अचेतन मस्तिष्कों द्वारा जो इन्द्रिय गम्य और अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध होता है उसका केन्द्र यही संस्थान है। ध्यान से लेकर समाधि तक और आत्म-चिन्तन से लेकर भक्तियोग तक की समस्त आध्यात्मिक साधनाएं यहीं से फलित और विकसित होती हैं। ओजस्, तेजस् और ब्रह्मवर्चस् के रूप में पराक्रम, विवेक एवं आत्मबल की उपलब्धियों का अभिवर्धन यहीं से उभरता है।
दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र दक्षिणी ध्रुव के समतुल्य जननेन्द्रिय मूल में अवस्थित ‘काम बीज’ है। इसी को साधना शास्त्र में मूलाधार चक्र कहा गया है। इसकी उपयोगिता और गरिमा अपने स्तर की है। मस्तिष्क ज्ञान का और काम बीज सामर्थ्य का उद्गम है। आत्मिक बल ऊपर है और भौतिक बल नीचे। भावनाएं, विचारणाएं आस्थाएं, ऊपर से उतरती हैं और पराक्रम, उत्साह, उल्लास नीचे से उभरता है। ऊर्ध्व केन्द्र को ब्रह्म का—अधः केन्द्र को प्रकृति का—सम्पर्क द्वार कह सकते हैं। अपने-अपने स्तर के आदान-प्रदान इन्हीं केन्द्रों से सम्भव होते हैं।
ऊर्ध्व क्षेत्र ग्रहण करता है और अधः क्षेत्र विसर्जन। शिरो भाग में मुख है जिससे अन्न, जल ग्रहण किया जाता है। नाक है, जिससे सांस ग्रहण की जाती है। कान सुनते, नेत्र देखते हैं। इनसे मस्तिष्क की ज्ञान सम्पदा बढ़ती है। यह शिर भाग ग्रहणकर्त्ता होने के कारण उत्तरी ध्रुव है। उसकी धुरी सहस्रार में है।
अधःक्षेत्र से विसर्जन होते प्रत्यक्ष देखा जाता है। मल, मूत्र, वीर्य का क्षरण इसी क्षेत्र से होता है। कामुकता यहीं से उठती है और मस्तिष्क की सरसता का प्रलोभन देकर अपने चंगुल में जकड़े रहती है। विवाह सन्तान का ताना बाना इसके चरखे कातने पर तैयार होता है। इन्हीं दो प्रयोजनों में जीवन—सम्पदा का अधिकांश भाग खर्च हो जाता है दक्षिणी ध्रुव से विसर्जन प्रक्रिया काम केन्द्र द्वारा किस प्रकार होती है यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है ओजस् का दिव्य उत्पादन शरीर में होता है उसे क्रमशः अधिक सूक्ष्म और विकसित करते रहा जाय तो मानसिक तेजस् और आत्मिक वर्चस् की अभिवृद्धि करते-करते मनुष्य प्रचण्ड पराक्रमी हो सकता है, पर वे सभी दिव्य विभूतियां इसी काम क्षेत्र के उभारों में होकर अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य साधने और इस संचय को कलात्मक एवं भावनात्मक दिव्य प्रयोजनों में लगा कर मनुष्य क्या नहीं बन सकता? किन्तु क्षरण के कारण तो वह खोखला ही बनता जाता है। सामान्य निर्वाह तक में कमी कठिनाई पड़ती है, तब महत्वपूर्ण पद्धति के लिए साधना सामग्री कैसे जुटे?
काम केन्द्र का यह एक अद्भुत चमत्कार है कि वहां से नये मनुष्य का जन्म अवतरण सम्भव होता है प्राणियों का उत्पादक परमात्मा है, पर जब जीव को अपने ही समतुल्य नया जीव बनाते देखा जाता है तो जी चाहता है कि उसे भी सृष्टा कहा जाय? अपने शरीर में से अपने जैसे नये-नये शरीर बना कर खड़े करते आना अनोखे किस्म का जादू है। जादूगर अपनी झोली, हथेली, मुख आदि से अन्य वस्तुएं तो निकालते हैं, पर अपने जैसा मनुष्य निकाल सकना उनमें से किसी के लिए भी सम्भव नहीं हो सका। यह जादू मनुष्य काया में स्थित काम केन्द्र का ही है जो ऐसा अद्भुत उत्पादन सम्भव बना देता है।
काम केन्द्र मात्र रति प्रेरणा ही नहीं उभारता। उसमें कला सौन्दर्य, उत्साह, उल्लास, साहस जैसी अनेकों सृजन सम्वेदनाएं उफनती रहती हैं। ‘नपुंसक’ शब्द एक प्रकार की गाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति राजकीय सेवा में स्वास्थ्य की दृष्टि से ‘अनफिट’ कर दिये जाते हैं। सेना, पुलिस जैसे साहसिक कार्यों में उनको प्रवेश नहीं मिलता। श्राद्ध और यज्ञ का संचालन करने में नपुंसक आचार्यों को बहिष्कृत ठहराया गया है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ‘क्लीव’ कहकर प्रकारान्तर से गाली ही दी थी। अध्यात्म क्षेत्र की नपुंसकता, नीरसता, निराशा, निष्क्रियता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इन प्रवृत्तियों में उभार या उतार की स्थिति बनने के लिए काम केन्द्र की स्थिति को उत्तरदायी माना गया है। सन्तानोत्पादन से लेकर सृजनात्मक क्षमताओं तक सम्बन्ध इसी केन्द्र से जुड़ता है। ऐसे-ऐसे अनेकों तथ्य मिलाकर यह सिद्ध करते हैं कि भौतिकी क्षमताओं और सफलताओं की दृष्ट से काम संस्थान का—मूलाधार चक्र का कितना महत्व है। जीव विकास विज्ञानियों ने तो प्रगति प्रेरणाओं को मनोविज्ञान के क्षेत्र में ‘सेक्स’ संज्ञा दी है। यहां रति कर्म को नहीं उत्साह और आनन्द के समन्वय को ही ‘सेक्स’ संज्ञक कहा गया है।
काम बीज का प्रतीक मूलाधार और ज्ञान बीज का प्रतिनिधि सहस्रार चक्र है। इन्हें, मानवी सत्ता के दो अति महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र कहा जा सकता है। यहां एक बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि इन्हें शरीर शास्त्र के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अवयव नहीं मानना चाहिए यह सभी सूक्ष्म शरीर में रहने वाली सत्ताएं हैं। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर से मिलते-जुलते अवयव पाये जाते हैं और उनके सहारे स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के बीच आदान-प्रदान भी होते रहते हैं। इतने पर भी दोनों के अस्तित्व एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। रक्त संचार की थैली भी हृदय है और सहृदयता एवं हृदय हीनता के रूप में विद्यमान अन्तरात्मा भी हृदय कहलाती है। हृदय गुफा में ध्यान करने के लिए कहा गया है। यह ‘हृदय’ रक्त शोधक थैली नहीं, वरन् सूक्ष्म शरीर में अवस्थित विशिष्ट चेतना केन्द्र है। ठीक इसी प्रकार मूलाधार एवं सहस्रार को प्रत्यक्ष शरीर का कोई अवयव विशेष नहीं मानना चाहिए। हां, उनसे मिलते-जुलते अवयवों का अस्तित्व किसी औंधे-तिरछे रूप में अवश्य पाया जा सकता है। उनका इतना ही महत्व है कि उन्हें झकझोरने से अधिष्ठात्री सूक्ष्म शक्ति को किसी कदर प्रभावित किया जा सकता है। साधना प्रयोजनों में इन अवयवों से भी कुछ न कुछ काम लिया जाता है। प्रगति पथ-प्रशस्त होने में इससे सहायता भी मिलती है।
कुण्डलिनी जागरण में मूलाधार और सहस्रार में अवस्थित भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों के पारस्परिक शिथिल सम्बन्ध को सघन बनाया जाता है। दोनों के बीच आदान-प्रदान की गति तीव्र की जाती है। इन दोनों सरोवरों के बीच सम्बन्ध मार्ग है—मेरुदण्ड। इसी को महामार्ग कहा गया है। महा प्रयाण की, ऊर्ध्वगमन की देवयान प्रक्रिया यही है। पाण्डवों के स्वर्गारोहण को—इसी प्रयास का अलंकारिक कथा प्रसंग कहना चाहिए।
कुण्डलिनी योग को भौतिक और आत्मिक प्रखरता प्राप्त करने की समर्थ साधना माना जाता है। पृथ्वी मूलाधार स्थित शरीरगत शक्ति, सूर्य ब्रह्मरन्ध्र स्थित सहस्रदल, कमल, इन दोनों के परस्पर सुयोग सम्मिलन का नाम ही कुण्डलिनी जागरण है। मूलाधार और सहस्रार के बीच पांच और दूसरे चक्र हैं। कुण्डलिनी शक्ति जो मूलाधार केन्द्र में अवस्थित रहती है इन पांचों चक्रों का बंधन करती हुई सहस्रार से जा मिलती है और फिर वे सभी परिणाम ऋद्धि सिद्धियां, वैभव ऐश्वर्य आ प्रस्तुत होते हैं जो कुण्डलिनी जागरण की सफलता समझे जाते हैं।
मूलाधार केन्द्र में अवस्थित कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए यों विविध विधि साधनात्मक क्रियाकलाप अपनाये जाते हैं। कर्मकांडों के साधनात्मक उपचारों के आधार पर साधकगण छहों चक्रों का वेधन कर कुण्डलिनी शक्ति को सहस्रार चक्र तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और इसके लिए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि आदि का सहारा लेते हैं। इन साधन प्रयोगों में मूलतः संकल्प शक्ति का ही उपयोग किया जाता है और प्रखर संकल्प बल के आधार पर मानवी काया में अवस्थित सप्त चक्रों के माध्यम से वे समस्त सिद्धियां हस्तगत की जाती हैं, जिनका उल्लेख योग-शास्त्रों में मिलता है।
मानवी संकल्प शक्ति की क्षमता असीम है। उसको जागृत करना और सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर सकना संभव हो सके तो कुछ भी बन सकना और कुछ भी कर सकना संभव हो सकता है—
फलं ददाति काले न तस्य तस्य तथा तथा
तपोवा देवता वाणी भूत्वा स्वैव रिन्यथा,
फलं ददात्यथ स्वैर नभः फलं निपातवत्,
तपोवा देवता वाणी भूत्वा स्वैव रिन्यथा,
फलं ददात्यथ स्वैर नभः फलं निपातवत्,
योगवशिष्ठ
‘‘जीव अपनी इच्छा से ही देवता, तपस्वी बनता रहता है। प्रगति और अवलति का आधार मनुष्य का अपना कर्तृत्व ही है।’’
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ।
सप्त रक्षति सर्व अप्रमादम् ।।
सप्त रक्षति सर्व अप्रमादम् ।।
यजु.
शरीर में सात ऋषि निवास करते हैं। वे सतर्कता पूर्वक उसकी निरंतर रक्षा करते हैं।
इस तथ्य की ओर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि समस्त संपदाओं और विभूतियों का केन्द्र मनुष्य के अपने ही भीतर निहित है शरीर के बाहर की ओर बनी इंद्रियां बाहर का तो बहुत कुछ देखती हैं पर आन्तरिक सम्पदा को समझने उसका सदुपयोग करने से वंचित ही रह जाती हैं। हमारी बुद्धि बाहरी समस्याओं को सुलझाने में तो लगी रहती है किन्तु जीव के स्वरूप, लक्ष्य एवं उपयोग को जानने में असमर्थ रहती है।
पराञ्चि खानि ब्यतृणत् स्वयम्भू स्तस्माद् पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृत- त्वमिच्छन्ं।।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृत- त्वमिच्छन्ं।।
(कठोपनिषद 2।4।1)
विधाता ने छेदों को बाहर की ओर छेदा (अर्थात् इन्द्रियों को बहिर्मुखी बनाया) अतएव मनुष्य बाहर ही देखता है। अन्तर को नहीं दीखता। अमृत की आकांक्षा करने वाला दूरदर्शी विरला मनुष्य ही अन्दर की ओर देखता है।
गायत्री की उच्चस्तरीय साधना में सप्त चक्रों का जागरण प्रमुख है। यह सप्त चक्र और पंचकोश परस्पर सम्बद्ध हैं। दोनों की साधना एक साथ ही सम्पन्न होती है। इसी में देव साधना, ऋषि उपासना- समग्र उत्कर्ष, जीवन-लक्ष्य, सर्वतोमुखी विकास उल्लास के समस्त तत्वों का समावेश है। कहा गया है—
मूलादि ब्रह्म रंध्रान्ता गीयते मननात् यतः ।
मननात् त्राति षट्चक्रं गायत्री लेन कथ्यते ।।
मननात् त्राति षट्चक्रं गायत्री लेन कथ्यते ।।
—तन्त्र कौमुदी
आत्मसत्ता में सन्निहित विश्व की समस्त विभूतियों को यदि खोजा और जगाया जा सके तो जीवात्मा को देवात्मा एवं परमात्मा बनने का अवसर मिल सकता है। इस अन्वेषण प्रयास को ब्रह्म विद्या और जागरण प्रक्रिया को ब्रह्म तेज सम्पादन कहते हैं। इस सन्दर्भ में सप्त ऋषियों को जीवन्त करने और उनके ब्रह्म-बल से उच्च कोटि का लाभ उठाने की प्रक्रिया ‘चक्रवेधन’ के रूप में समझी जा सकती है।
चक्रवेधन के लिए किये जाने वाले क्रिया कलाप यदि क्रिया-कृत्य ही सीमित रहे—उनमें संकल्प शक्ति का कोई पुट न दिया जाय तो इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प शक्ति के उपयोग एवं प्रयोग के साथ-साथ भावनात्मक स्तर पर भी अनुकूलता एवं अनुरूपता विनिर्मित करनी पड़ेगी। पृथ्वी अर्थात् भौतिक सम्पदा-अहंता, सूर्य अर्थात् आत्मिक सत्ता ब्रह्म चेतना इन दोनों को जो जितना जोड़ जा सकता है उसे कुण्डलिनी जागरण के साथ जुड़ी हुई विभूतियां मिलती हैं। स्वार्थ को परमार्थ में जोड़ने का, शारीरिक वासनाओं को आत्मिक उल्लासों में घुला देने का नाम ही आत्म समर्पण है। इसी को साधना क्षेत्र में पृथ्वी और और सूर्य का संयोग कहते हैं। कुण्डलिनी साधना इसी केन्द्र बिन्दु पर पहुंचने की चेष्टा को कह सकते हैं।
अशक्तता और संकीर्णता एक ही तथ्य के दो नाम हैं। कुण्डलिनी साधना द्वारा भीतर भरे शक्ति स्रोत को उभारा जाता है। और निखिल ब्रह्माण्ड में संव्याप्त अनन्त सामर्थ्य को अपने भीतर धारण किया जाता है। यह धारणा ही वह पात्रता है जिसके आधार पर दिव्य शक्तियों का साधक में अवतरण होता है। शारीरिक और मानसिक साधना पद्धति की उपयोगिता भी है और आवश्यकता भी। पर उसकी पूर्णता तभी होती है, जब अपने अणु अस्तित्व को विराट् के विभु में समर्पित कर दिया जाय। यह समर्पण जितना यथार्थ और जितना प्रगाढ़ होता है, उसी अनुपात से सफलता का पथ प्रशस्त होता चला जाता है।
कुण्डलिनी शक्ति एक होते हुए भी व्यक्ति तथा संसार के चेतन और जड़ जगत के अनेक प्रयोजन पूरे करती है। बिजली घर में विनिर्मित होने वाले विद्युत भण्डार का संग्रह एक ही प्रकार का है पर उसके द्वारा बत्तियां, पंखे, हीटर, कूलर, रेडियो आदि के अनेक घरेलू प्रयोजन पूरे होते हैं और अनेक तरह के कल कारखाने चलते तथा अगणित प्रकार का उत्पादन करते हैं। इन क्रिया कलापों के नाम रूप अनेक हैं। उनके वाह्य स्वरूपों की भिन्नता इतने अधिक प्रकार और स्तर की है कि किसी का किसी से कोई सीधा सम्बन्ध मालूम नहीं पड़ता। पंखा चलाने और रेडियो बजने के वाह्य स्वरूप में भारी अन्तर मालूम पड़ता है। एक मशीन से सिंचाई के लिए पानी निकलता है और दूसरी लोहा गलाने की भट्टी जलाती है। दोनों में प्रत्यक्षतः कितना भारी अन्तर दीखता है, पर बारीकी से देखने पर एक ही विद्युत भण्डार के यह विविध विधि क्रिया कलाप सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार कुण्डलिनी शक्ति एक विश्व व्यापी जीवन प्राण और समर्थ क्षमता के रूप में एक ही प्रकार की है पर उसके कार्य जड़ जगत में अलग प्रकार के और चेतन जगत में अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं।
चेतन जगत में इसकी क्रियाशीलता प्राणियों के जन्म, अभिवर्धन, वृद्धावस्था, मृत्यु तथा अंग प्रत्यंगों की दृश्य एवं अदृश्य गति-विधियों के रूप में देखी जा सकती है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव, संस्कार आदि के रूप में उसी महाशक्ति का प्रकाश फैला हुआ देखा जा सकता है। पंचतत्वों के विभिन्न सम्मिश्रणों चेतनाओं के अनेक विभाजनों का एकत्रीकरण तथा कर्म संस्कारों के योग से जो अगणित योनियों में जन्म लेने वाले असंख्य आकृति प्रकृति के जीव उत्पन्न होते हैं उनमें यह कुण्डलिनी शक्ति की चेतन जगत में चल रही गति विधियां ही कारण है, जड़ जगत में पृथ्वी और आकाश में जो विदित और अविदित अनेक हलचलें उत्पन्न होती रहती हैं और परिवर्तनों से भरी चंचलता निरन्तर गतिवान रहती है, उसका कारण भी दिव्य सत्ता है। अणु परमाणुओं की द्रुतगामी हलचलों से लेकर ग्रह नक्षत्रों का चल वल, समुद्र के ज्वार भाटे, भूकम्प, ऋतु परिवर्तन, भू-गर्भ के अन्तरंग में निरन्तर चल रहे हेर फेर, ईथर तत्व की सक्रियता आदि जड़ जगत में चल रही समस्त उथल-पुथल के पीछे यह कुण्डलिनी शक्ति ही काम करती है। उनका क्रिया-कलाप एक क्षण के लिए भी बन्द हो जाय तो महा प्रलय ही सामने होगी। तब यहां सब कुछ निर्जीव, नीरस, निष्क्रिय नितान्त नीरव और अन्धकार ही यहां शेष रह जायेगा। सम्भवतः तब सारी आकृतियां बिगड़ कर पुनः नीहारिकाएं उत्पन्न करने वाली धूमिलता में ही बिखर जायें और देखने अनुभव करने जैसा कुछ शेष ही न रह जाय।
लकड़ी का टुकड़ा यदि अग्नि जैसा तेजस्वी बनना चाहता हो तो उसे अग्नि रूप बनने के लिए वर्तमान अस्तित्व गंवाना ही पड़ेगा बीज अपना अस्तित्व भी न खोना चाहे और विशाल वृक्ष बनने का लाभ भी लेना चाहे तो यह दोनों बातें न हो सकेंगी। संकीर्णता और आत्मिक प्रगति का जोड़ा मिल ही नहीं सकता। जो जितना स्वार्थी है उसे आत्मिक प्रगति के पथ पर चलते हुए उतनी ही कठिनाई अनुभव होगी। आत्मिक सिद्धियां हैं, तो पर उनका लाभ कृपणता और स्वार्थ परता के रहते उठाया नहीं जा सकता। जीवन साधना का तात्पर्य ही अहंता का विसर्जन है। पारमार्थिक दृष्टिकोण अपनाये बिना न जीवन लक्ष्य पूरा होता है और न कुण्डलिनी जागरण जैसी योग साधनाओं में सफलता मिलती है।
आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करने का मतलब है व्यष्टि को समष्टि से सम्बन्ध बनाते उसे घनिष्ठ करते हुए अन्ततः परस्पर दोनों का एक हो जाना। एक का दूसरे में विलीन हो जाना। जीवात्मा वस्तुतः विश्वात्मा—परमात्मा का ही एक अंग है। जो जिसका अंग है वह उसी में लीन होने को व्याकुल रहता है और जब तक वह प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता तब तक बेचैन ही रहता है। जल का भण्डार समुद्र है। समुद्र से ही बादल निकल कर सर्वत्र जल बरसाते हैं। यह बरसाया हुआ जल नदी, नाले झरने, तालाब, पृथ्वी के भीतर की नालियों आदि में होता हुआ यह प्रयत्न करता है कि वह समुद्र में जाकर मिले। जिधर भी पानी को ढलान दीखती है, उधर ही बहने लगता है। इस ढलान और प्रवाह का प्रयोजन उस बिखरे हुए जल अंशों को अपने मूल भण्डार समुद्र तक पहुंचा देना ही है। आत्मिक उन्नति का उद्देश्य जीव की इस गति में तीव्रता ला देता है जिसके आधार पर वह एक छोटा, टुकड़ा न रह कर अपने उद्गम में जा मिले और अपूर्णता खोकर पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर ले।
लेकिन अधिकांश लोग अधोगामी प्रवृत्ति ही अपनाये रहते हैं। पुराणों में ऐसे व्यक्तियों को पतित कह गया है। जिसका आशय है कि प्रगति ऊर्ध्व गमन को कहते हैं तथा पतन को अधोगमन कहा जाता है। मूलाधार गत शरीर चेतना-साधन शक्ति जब ऊर्ध्व गमन की इच्छा करती है तो उसे सहस्रार की ओर उठना, चलना पड़ता है। काम बीज का ज्ञान बीज में परिवर्तन, विसर्जन, समर्पण करने की प्रक्रिया ही आत्मिक प्रगति का—लक्ष्य प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है।
इस आत्मिक उत्कर्ष के अनेकों मार्ग हो सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थ परता के बन्धनों को शिथिल रहने और तोड़ने का प्रत्येक प्रयास इसी स्तर का माना जायेगा। जिन विचारों, योजनाओं और गतिविधियों में आदर्शवादी सिद्धान्तों को अपनाने की बात बनती हो उन्हें; आत्मोत्कर्ष की साधना का एक स्वरूप माना जा सकता है। कुंडलिनी जागरण उसी प्रकार की वैज्ञानिक परिपाटी के आधार पर परिणाम प्रस्तुत करने वाली साधना है। इसमें शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों के महत्व पूर्ण आधार जुड़े हुए हैं। भौतिकी और ब्रह्मविद्या के दोनों तत्वों का इसमें समान रूप से समावेश है।
जीवसत्ता सामान्यतया शरीराध्यास में डूबी रहती है। इसी वस्तुस्थिति का चित्रण कुण्डलिनी ज्ञान में इस प्रकार किया गया है। कि मूलाधार क्षेत्र में एक महासर्पिणी किसी लिंग प्रतीक से साढ़े तीन लपेटे मार का सोई हुई है। उसका मुख नीचे की ओर है और उससे विष झरता है। यह लिंग कन्द-संसार का अकर्षण है। जीव-सत्ता सर्पिणी है। वह आत्मबोध के सम्बन्ध में प्रसुप्त स्थिति पड़ी है। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान है, न लक्ष्य का मोह मदिरा पीकर वह अज्ञान की मूर्च्छा से ग्रसित हो रही हैं। साड़े तीन फेरो में तीन तो वासना, तृष्णा और अहंता के पूरे हैं। बीच-बीच में कभी-कभी आत्म-कल्याण की बात भी हलके-फुलके ढंग से उभरती है। अन्तरात्मा की यह पुकार पूरी तरह कोई भी कुचल नहीं सकता। वह अपनी मांग करती ही रहेगी, भले ही उसे पग-पग पर अनसुनी किया जाता रहे। यही है आधा लपेट जिसे मिलाकर साड़े तीन फेरे बनते हैं। सुप्त-प्रसुप्त कुण्डलिनी का मुख नीचे की ओर अधःपतन की ओर है। हमारी निकृष्ट आकांक्षाएं और प्रवृत्तियां आत्म-कल्याण से नीचे ही धकेलने वाली बन गई हैं। शक्तियों का क्षरण—अधोमुखी बना हुआ है। वीर्यपात से लेकर अन्य कार्य भी उठाने वाले नहीं, गिराने वाले ही बने हुए हैं। उनके दुष्परिणाम विष तुल्य होते हैं। जीवसत्ता की दुर्गति का चित्रण प्रसुप्त सर्पिणी के रूप में किया गया है तो यह उचित ही है। हमारी सत्ता इस विश्व वसुधा में सर्पिणी के समतुल्य ही हेय बनकर रह रही है। हमारे उत्पादन विष तुल्य ही हैं। विष बीज बोने और विषाक्त प्रदूषण फैलाने वाली ही तो अपनी जीवन प्रक्रिया बन रही है। मोह मदिरा पीकर उन्मत्त बने दुर्भाग्य-ग्रस्त मनुष्यों की तरह ही अपनी स्थिति बनी हुई है।
कुण्डलिनी जब जागती है तो प्रसुप्ति छोड़ती है। लपेटे खोल देती है। तन कर खड़ी हो जाती है। मेरुदण्ड मार्ग से ऊपर की ओर चढ़ना प्रारम्भ करती है। उसके मुख से विषाक्त दुर्गन्ध के स्थान पर अमृतमयी सुगन्ध के श्वास निकलने लगते हैं। यह दृश्य आत्मोत्थान की ओर उन्मुख होने का है। कुण्डलिनी मेरुदण्ड मार्ग से ऊपर चलती है और सहस्रार अवस्थित महासर्प से जा लिपटती है। इसे शिव-पार्वती विवाह की कथा—गाथा के रूप में समझाने का प्रयत्न किया गया है। सती-शिव से विमुख होकर पिता के घर गई थीं और खिन्न होकर अग्निकुण्ड में जल मरी थीं। यह आत्मा का परमात्मा से विमुख होकर नारकीय यातनाओं के कुण्ड में जल मरना है। स्थिति बदलती है। सती नया जन्म पार्वती के रूप में लेती हैं। तप करती है और शिव की अर्धांगिनी बन जाती हैं। यह जीवसत्ता का योग तप की साधना अपनाकर अपनी पात्रता को विकसित करना और ऊर्ध्वगामी बनकर परमात्मा में समन्वित हो जाने का विकास क्रम है। कुण्डलिनी जागरण साधना का तत्वदर्शन इन कथानकों के माध्यम से अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है।
समुद्र मन्थन की कथा भी प्रकारान्तर से कुण्डलिनी जागरण प्रक्रिया का ही दिग्दर्शन है। समुद्र मन्थन की कथा में जीव की वस्तुस्थिति और कुण्डलिनी जागरण साधना से उसकी प्रगति सद्गति का अच्छा खासा चित्रण है। कूर्म अर्थात् भगवान्—पैर समेटे—गई-गुजरी स्थिति सबसे नीचे। मन्थन के लिए लाया गया मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर। मथने के कार्य में प्रयुक्त होने वाली वासुकी सर्प की रज्जु। देवता और असुरों द्वारा उसका मन्थन। यही है समुद्र मन्थन का दृश्य चित्र। हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर का स्थान सबसे नीचे है। वह कुछ करा सकने की स्थिति में नहीं है। कछुए की तरह सिकुड़ा-सिमटा ज्यों-त्यों करके मानवी-सत्ता का भार वहन कर रहा है। मंदराचल—वैभव। मदिरा (मादक) अचल (संग्रहीत)। अपना धन, वैभव, उद्धत अहंता की तृप्ति में तथा अचल (संग्रह) करने के लिए प्रयुक्त होता है। वासुकी सर्प—विषधर जीव। साड़े तीन लपेटों से मदिराचल के साथ लिपटा है और दोनों दिशाओं में देव-दानवों द्वारा घसीटे जाने के कारण दुर्दशाग्रस्त हो रहा है। हड्डी-पसलियों का कचूमर निकला जा रहा है। इस चित्रण में हम अपनी दुर्दशा का चित्र तथा भावी प्रगति का उपाय आभास देखने का दुहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जीवन-क्रम में संव्याप्त जड़ता को—पशु-प्रवृत्तियों के अभ्यस्त प्रवाह को निरस्त किया जाना चाहिए। चिन्तन में समुद्र मन्थन जैसी प्रखरता उत्पन्न की जाती चाहिए। प्रसुप्ति को जागृति में—मूर्छना को क्रान्तिकारी परिवर्तन में परिणत करने की आवश्यकता है। जीवन मन्थन कर डाला जाय—काया-कल्प के लिए कटिबद्ध हुआ जाय। पशु-प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर देवयान के पथ पर चलने का साहस जुटाया जाय तो अपने लिए भी समुद्र मन्थन से उपलब्ध हुए बहुमूल्य रत्नों की तरह अति महत्वपूर्ण उपलब्धियां करतलगत हो सकती हैं। व्यामोह की, प्रलोभनों की, उन्मादों की सनकें यदि अन्तःचेतना पर छाई ही रहीं, अन्तर्द्वन्दों में क्षमता का अपव्यय होता रहा तो इस जीवन व्यापार में कमाया कुछ न जा सकेगा। जो पूंजी साथ लेकर आये थे वह भी गंवा कर ऋण भार लाद कर वापिस जाना पड़ेगा। इस स्थिति से बचने के लिए जीवन मन्थन आवश्यक है। क्रान्तिकारी परिवर्तन अभीष्ट है। समुद्र मन्थन की कथा की मन्थन प्रक्रिया को कुण्डलिनी जागरण पद्धति के साथ सहजभाव से जोड़ा जा सकता है।
कामनाएं भावनाओं में परिणित होने के लिए संकल्प करती हैं तो उनकी स्थिति गंगा के समुद्र विलय होने की आतुरता जैसी बन जाती है। हिमालय से निकल कर गंगा आतुरतापूर्वक समुद्र मिलन के लिए लम्बा मार्ग पार करती हुई दौड़ती है। कुण्डलिनी को गंगा—मेरुदण्ड मार्ग को प्रवाह पथ और सहस्रार को समुद्र कहा जा सकता है। अपने प्रियतम को पाकर गंगा ने अशान्ति से छुटकारा पाया और महान् से मिलकर महान् बन गई।
नर को नारायण बनने में तभी सफलता मिले जब वह अनन्त चेतना के दिव्य शक्तिस्रोत सविता देवता से अपने सम्बन्ध जोड़ेगा। सूर्य कितना तेजस्वी है, कितना समर्थ है यह जानने वाला सूर्य पुत्र बनने के लिए उसकी साधना कुण्डलिनी योग द्वारा करते तो हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अपनी सत्ता में दिव्य चेतना भी उसी मार्ग पर चलते हुए प्रखर बनानी होगी, जिस पर चलते हुए एक तुच्छ सा अग्निपिण्ड सविता के रूप में विकसित हुआ है।