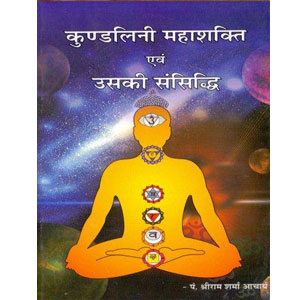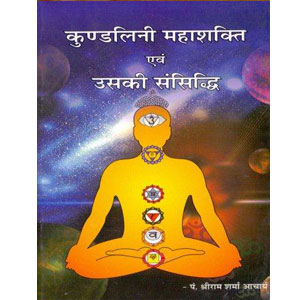कुण्डलिनी महाशक्ति और उसकी संसिद्धि 
कुंडलिनी महाशक्ति की पौराणिक व्याख्या
Read Scan Versionआत्म विद्या के विद्यार्थियों को यह तो विदित ही रहता है कि वह मानवीय पिण्ड (शरीर) विश्व ब्रह्माण्ड का एक छोटा सा नमूना मात्र है। सूर्य चलता है और सौर मण्डल के ग्रह उपग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार परमाणु भी अकेला नहीं होता, उसके साथ इलेक्ट्रोन, प्रोट्रॉन, न्यूट्रोन आदि की एक मण्डली रहती है जो ‘न्युक्लियस’ से प्रभावित होकर अपना कार्य उसी तरह चलाती है जिस तरह सौर मण्डल के साथ। विशाल वृक्ष का सारा ढांचा छोटे से बीज के भीतर पूरी तरह विद्यमान रहता है। मनुष्य का शरीर ही नहीं उसका स्वभाव, बुद्धि, अन्तःकरण आदि महत्व पूर्ण सूक्ष्म चेतना संस्थान भी अति सूक्ष्म रज वीर्य में पूरी तरह ‘‘जीन्स रूप से विद्यमान रहता है। ब्रह्माण्ड की विशाल व्यापकता को यदि हम बीज रूप में देखना चाहें तो उसे मानव शरीर की सूक्ष्मता का विश्लेषण करते हुए भली प्रकार जान सकते हैं। जान ही नहीं सकते उस व्यक्तिगत सूक्ष्मता का विश्व गरिमा के साथ जुड़े हुए अविच्छिन्न सम्बन्ध का लाभ भी उठा सकते हैं। यह सम्बन्ध सूत्र यदि प्रसुप्त न रह कर जागृत हो जाय, दुर्बल न रह कर परिपक्व हो जायें तो विश्व व्यापी शक्ति भण्डार से अपने लिए आवश्यक वस्तुयें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आकर्षित कर सकता है इतना ही नहीं? अपनी दुर्बल इकाई को समर्थ बनाकर उससे विराट् विश्व के जड़ चेतना संस्थान को प्रभावित कर सकता है।
साधना और तपश्चर्या वस्तुतः इसी अति महत्व पूर्ण विज्ञान का नाम है। प्राचीन काल में तप साधना के द्वारा जिनने जो वरदान पाये थे उनके इतिहास, पुराण विस्तार पूर्वक हम पढ़ते सुनते हैं। इन दिनों वैसी उपलब्धियां प्रत्यक्ष न होने से वे बातें कपोल कल्पना जैसी लगती हैं; पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। यदि ठीक विधि से—ठीक उपकरणों द्वारा उस विज्ञान को कार्यान्वित किया जाय तो पूर्व काल की कपोल कल्पना समझी जाने वाली बातों को आज भी प्रत्यक्ष किया जाना सम्भव है।
तपस्वियों द्वारा साधना के फलस्वरूप प्राप्त किये वरदान और कुछ नहीं विराट् विश्व की अन्तरंग शक्तियों में से कुछ का इच्छानुकूल उपयोग कर सकने की क्षमता ही समझी जानी चाहिए इसी प्रकार शाप वरदान दें सकने की क्षमता को अपनी व्यक्तिगत इकाई को इतना प्रबल बना लेना चाहिए जिससे मनुष्यों या पदार्थों को अपनी संकल्प शक्ति के प्रहार से अभीष्ट दिशा में मुड़ने के लिए विवश किया जा सके। देवताओं का अस्तित्व इस विराट् विश्व में उनकी विशालता के अनुरूप व्यापक भी हो सकता है? पर हम से देवताओं के जिस अंश का प्रत्यक्ष और सीधा सम्बन्ध है वह अंश अपने भीतर ही ‘शक्ति बीजों’ के रूप में विद्यमान रहता है। साधना का प्रयोजन इन्हीं शक्ति बीजों को जागृत और समर्थ बनाना है। समष्टिगत देवताओं का आशीर्वाद, वायु, वर्षा, धूप, शीत, दुर्भिक्ष, सुभिक्ष आदि के रूप में समग्र रूप से बरसता है और उससे सबको समान लाभ मिलता है। व्यक्तिगत वरदान आशीर्वाद देने वाले देवता अपने शरीर में ही विद्यमान रहते हैं। विविध-विधि साधनाओं द्वारा उन्हीं को स्वयं समर्थ बनाया जाता है और अपनी पात्रता एवं तपस्या के अनुरूप उन्हीं से वह लाभ पाया जाता है जिसे ‘अलौकिक चमत्कारी’ देव प्रदत्त, वरदान के रूप में आश्चर्य के साथ सुना और देखा जाता है।
इस अलौकिक और अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत करने वाली शक्ति को ही योगियों और तपस्वियों ने कुंडलिनी नाम दिया है और उसे जीवन चेतना का आधार बताया है। उसी से जीवधारियों को शक्ति और तेजस्विता मिलती है, सामान्य स्थिति में व्यक्ति की कुण्डलिनी शक्ति जितनी मात्रा में स्पन्दन करती है, उतना ही प्रभाव क्षेत्र, उस मनुष्य का होता है। उसी के आधार और अनुपात से लोगों को सुख-दुःख आदर-सम्मान, लोक प्रतिष्ठा आदि मिलती है। इसलिए कहना न होगा कि मनुष्य के स्थूल जीवन की नहीं व्यावहारिक जीवन की सफलता और समुन्नति का आधार भी कुण्डलिनी शक्ति ही है।
पांचों प्रकार की ज्ञान इन्द्रियां भी बिजली के तारों की तरह इसी परमशक्ति से जुड़ गई हैं, इसलिए वह सूक्ष्म चेतना होने पर भी संकल्प रूप में आ गई है। चेतन होने के कारण चिति, जीने से जीव मनन करने से मन और बोध प्राप्त करने से चेतना को बुद्धि रूप में देखा जाता है। अहंकार रूप में उसे ही तुर्यष्टक कहते हैं पर इन विभिन्न नामों का एक ही आधार है चेतना। इस चेतना की, शक्तियों की मूलाधार शक्ति को ही कुण्डलिनी कहा जाता है। ज्ञान और अनुभव के पांचों कोश बीज रूप से इसी में पाये जाते हैं, इसलिए कुण्डलिनी शक्ति जागृत कर लेने वाला इन्द्रियों को उसी तरह वश में कर लेता है, जिस तरह लगाम लगे हुए घोड़ों को वश में कर लिया जाता है। जिसने इन्द्रियों को जीत लिया संसार में उसको किस का भय। जो निर्भय हो गया वही विश्व-विजेता हो गया।
कुण्डलिनी की इन्हीं महान् सामर्थ्यों को जान कर ही योग शास्त्रों में उसे सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसके साथ अनेक प्रकार की कल्पनायें जोड़ दी गई हैं। अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है। सीधे सरल शब्दों में कुण्डलिनी वह दिव्य मानस तेज है, जो आत्म-चेतना से परिसिक्त है और शरीर भर में व्याप्त है। साधना के फलस्वरूप यह तेज सिमट कर ध्यान के समय ज्योति बन कर देह में कार्य करने लगता है।
कुण्डलिनी शक्ति को और अच्छी तरह समझने के लिए श्वांस क्रिया और सुषुम्ना शीर्षक (मेडुला आफ लोंगलेटा) का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी तक इतना ही जान पाये हैं कि नाक से ली हुई सांस गले से होती हुई फुफ्फसों (फेफड़ों) तक पहुंचती है। फेफड़ों के छिद्रों में भरे हुये रक्त को वायु शुद्ध कर देती है और रक्त-परिसंचालन की गतिविधि शरीर में चलती रहती है।
किन्तु प्राणायाम द्वारा श्वांस-क्रिया को बन्द करके भारतीय योगियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चेतना जिस प्राण-तत्व को धारण किये हुए जीवित है, उसके लिए श्वांस-क्रिया आवश्यक नहीं। सांस ली हुई हवा का स्थूल भाग ही रक्त शुद्धि का काम करता है, उसका सूक्ष्म भाग सुषुम्ना शीर्षक में अवस्थित इड़ा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से नाभि-कन्द स्थिति चेतना को उद्दीप्त किये रहता है। ‘गोरक्ष पद्धति’ में श्लोक 48 में इस क्रिया को शक्तिचालन महामुद्रा, नाड़ी शोधन आदि नाम दिये हैं और लिखा है कि सामान्य अवस्था में इड़ा और पिंगला-नाड़ियों का शरीर की जिस ग्रन्थि या इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है, मनुष्य उसी प्रकार के विचारों से प्रभावित होता रहता है, इस अवस्था में नाड़ियों के स्वतः संचालन का अपना कोई क्रम नहीं होता। किन्तु जब विशेष रूप (प्राणायाम) से प्राणवायु को धौंका जाता है तो इड़ा (गर्म नाड़ी) और पिंगला (ठण्डी नाड़ी) सम-स्वर में प्रवाहित होने लगती हैं। इस अवस्था में विकास के साथ-साथ नाभि-कन्द में प्रकाश स्वरूप गोला भी विकसित होने लगता है। उससे प्राण शक्ति का विद्युत-शक्ति के समान निसृण होता है चूंकि सभी नाड़ियां इसी भाग से निकलती हैं इसलिए वह इस ज्योति गोले के संस्पर्श में होती हैं। सभी नाड़ियों में वह विश्वव्यापी शक्ति झरने से सारे शरीर में वह तेज ‘ओजस’ के रूप में प्रकट होने लगता है। इन्द्रियों में वही बल के रूप में, नेत्रों में चमक के रूप में परिलक्षित होता है। इस प्राण-शक्ति के कारण प्रबल आकर्षण शक्ति पैदा होती है।
यह शक्ति नाभि प्रदेश में प्रस्फुटित होती है और चूंकि कटि प्रदेश में भी उसी के समीप है, इसलिए वह भाग अधिक शीघ्र और तेजी से प्रभावित होता है। इसलिये यौन-शक्ति केन्द्रों को नियन्त्रण में रखना अधिक आवश्यक होता है। साधना की अवधि में संयम पर इसीलिए अधिक जोर दिया जाता है, जिससे कुण्डलिनी शक्ति का फैलाव ऊर्ध्वगामी हो जाये उसी से औज की वृद्धि होती है।
स्थूल रूप से शरीर के स्नायु मंडल को ही पाश्चात्य वैज्ञानिक देख पाये हैं, वे अभी तक नाड़ियों के भीतर बहने और गतिविधियों को मूलरूप से प्रभावित करने वाले प्राण प्रवाह को नहीं जान सके। स्थूल नेत्रों से उसे देखा जाना सम्भव भी नहीं है। उसे भारतीय योगियों ने चेतना के अति सूक्ष्म-स्तर का वेधन करके देखा। योग शिखोपनिषद में 101 नाड़ियों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने सुषुम्ना शीर्षक को परनाड़ी बताया है। यह कोई नाड़ी नहीं है वरन् इड़ा और पिंगला के समान विद्युत-प्रवाह से उत्पन्न हुई एक तीसरी धारा है जिसका स्थूल रूप से अस्तित्व नहीं भी है और सूक्ष्म रूप से इतना व्यापक एवं विशाल है कि जीव की चेतना जब उसमें से होकर भ्रमण करती है तो ऐसा लगता है कि वह किसी आकाश गंगा में प्रवाहित हो रहा हो। वहां से विशाल ब्रह्माण्ड की झांकी होती है। अन्तरिक्ष में अवस्थित अगणित सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह-नक्षत्र की स्थिति समझने और विश्व-व्यापी हलचलों को नाद रूप में सुनने-समझने का अलभ्य अवसर, जो किसी चन्द्रयान या राकेट के द्वारा भी सम्भव नहीं है, इसी शरीर में मिलता है। उस स्थिति का वर्णन किया जाये तो प्रतीत होगा कि कुछ स्थूल और सूक्ष्म इस संसार में विद्यमान् है उस सब के साथ सम्बन्ध मिला लेने और उनका लाभ उपलब्ध करने की क्षमता उस महान् आत्म-तेज में विद्यमान् है, जो कुण्डलिनी के भीतर बीज रूप में मौजूद है।
सुषुम्ना नाड़ी (स्पाइनलकार्ड) मेरुदण्ड में प्रवाहित होती है और ऊपर मस्तिष्क के चौथे खोखले भाग (फोर्थवेन्ट्रिकल) में जाकर सहस्रार चक्र में उसी तरह प्रविष्ट हो जाती है। जिस तरह कि तालाब पानी में से निकलती हुई कमल नाल से शत-दल कमल विकसित हो उठता है। सहस्रार चक्र ब्रह्माण्ड लोक का प्रतिनिधि है, वहां ब्रह्म की सम्पूर्ण विभूति-बीज रूप से विद्यमान् है और कुण्डलिनी की ज्वाला वहीं जाकर अन्तिम रूप से जा ठहरती है, उस स्थिति में निरन्तर मधुपान का सा, सम्भोग की तरह का सुख (जिसका कभी अन्त नहीं होता) है, उसी कारण कुण्डलिनी शक्ति से ब्रह्म प्राप्ति होना बताया जाता है।
कुण्डलिनी का महत्व इसी शरीर में परिपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का स्वामी बन कर आत्मा की अनुभूति और ईश्वर दर्शन प्राप्त करने से निःसन्देह बहुत अधिक बढ़ जाता है। पृथ्वी का आधार जिस प्रकार शेष भगवान को मानते हैं, उसी प्रकार कुण्डलिनी का शक्ति पर ही प्राणि मात्र का जीवन अस्तित्व टिका हुआ है। सर्प के आकार की वह महाशक्ति ऊपर जिस प्रकार मस्तिष्क में अवस्थित शून्य-चक्र से मिलती है, उसी प्रकार नीचे वह यौन-स्थान में विद्यमान् कुण्डलिनी के ऊपर टिकी रहती है। प्राण और अपान वायु के धौंकने से वह धीरे-धीरे मोटी, सीधी, सशक्त और परिपुष्ट होने लगती है। साधना की प्रारम्भिक अवस्था में यह क्रिया धीरे-धीरे होती है, किन्तु साक्षात्कार या सिद्धि की अवस्था में वह सीधी हो जाती है और सुषुम्ना का द्वार खुल जाने से शक्ति का स्फुरण वेग से फूट कर सारे शरीर में—विशेष रूप से मुखाकृति में—फूट पड़ता है। कुण्डलिनी जागरण दिव्य ज्ञान, दिव्य अनुभूति और अलौकिक सुख का सरोवर इसी शरीर में मिल जाता है।
सुषुम्ना नाड़ी का रुका हुआ छिद्र जब खुल जाता है तो साधक को एक प्रकार का अत्यन्त मधुर नाद सुनाई देने लगता है। यह ध्वनि प्रारम्भ में मेघ के गर्जन, वर्षा समुद्र की हहराहट, घण्टा, झांझ, वीणा और भ्रमर गुंजार के तुल्य विकसित होती है, यही बात में अनहद नाद में परिणित हो जाता है। नाभि से 4 अंगुल ऊपर यह आवाज सुनाई देती है, उसे सुन कर चित्त उसी प्रकार मोहित होता है जिस प्रकार वेणुनाद सुन कर सर्प सब कुछ भूल जाता है। अनहद नाद से साधक के मन पर चढ़े हुए जन्म-जन्मान्तरों के कुसंस्कार छूट जाते हैं।
कुण्डलिनी महाशक्ति को तन्त्र शास्त्रों में द्विमुखी सर्पिणी कहा गया है। उसका एक मुख मल-मूत्र इन्द्रियों के मध्य मूलाधार चक्र में है। दूसरा मुख मस्तिष्क के मध्य ब्रह्म रन्ध्र में। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में सन्निहित महान् शक्तियों का परस्पर आदान प्रदान निरन्तर होता रहता है, इसी से इस पृथ्वी का सारा क्रिया-कलाप यथाक्रम चल रहा है। इसी प्रकार कुण्डलिनी शक्ति के ऊपर और नीचे के—जननेन्द्रिय और मस्तिष्क अधःऊर्ध्व केन्द्रों की शक्तियों का निरन्तर आदान-प्रदान होता रहता है। यह संचार क्रिया मेरु-दण्ड के माध्यम से होती है। रीढ़ की हड्डी इन दोनों केन्द्रों को परस्पर मिलाने का काम करती है। वस्तुतः स्थूल कुण्डलिनी का महासर्पिणी स्वरूप मूलाधार से लेकर मेरु-दण्ड समेत ब्रह्म-रन्ध्र तक फैले हुए सर्पाकृत कलेवर में ही पूरी तरह देखी जा सकती है। ऊपर नीचे मुड़े हुए दो महान् शक्तिशाली केन्द्र चक्र ही उसके आगे पीछे वाले दो मुख हैं।
मेरु-दण्ड पोला है, उसके भीतर जो कुछ है, उसकी चर्चा शरीर शास्त्र के स्थूल प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर दूसरे ढंग से की जा सकती है। शल्य क्रिया द्वारा जो देखा जा सकता है, वह रचना क्रम दूसरा है। हमें सूक्ष्म प्रक्रिया के अन्तर्गत योग-शास्त्र की दृष्टि से इस परिधि में सन्निहित दिव्य शक्तियों की चर्चा करनी है। योग-शास्त्र के अनुसार मेरु-दण्ड में एक ब्रह्म नाड़ी है और उसके अन्तर्गत इड़ा और पिंगला दो अन्तर्गत शिरायें गतिशील हैं। यह नाड़ियां रक्त वाहिनी शिरायें नहीं समझी जानी चाहियें। वस्तुतः ये विद्युत धारायें हैं। जैसे बिजली के तार में ऊपर एक रबड़ का खोल चढ़ा होता है और उसके भीतर जस्ते तथा तांबे का ठंडा गरम तार रहता है, उसी प्रकार इन नाड़ियों को समझा जाना चाहिए। ब्रह्म-नाड़ी रबड़ का खोल हुआ, उसके भीतर इड़ा और पिंगला ठंडे-गरम तारों की तरह हैं। इनका स्थूल कलेवर या अस्तित्व नहीं है। शल्य-क्रिया द्वारा यह नाड़ियां नहीं देखी जा सकतीं। इस रचना क्रम को सूक्ष्म विद्युत धाराओं की दिव्य रचना ही कहना चाहिए।
मस्तिष्क के भीतरी भाग में यो कतिपय कोष्ठकों के अन्तर्गत भरा हुआ मज्जा भाग ही देखने को मिलेगा। खुर्दबीन से और कुछ देखा नहीं जा सकता पर सभी जानते हैं, उस दिव्य संस्थान के नगण्य से दीखने वाले घटकों के अन्तर्गत विलक्षण शक्तियां भरी पड़ी हैं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व, सारा चिन्तन, सारा क्रिया कलाप और सारा शारीरिक, मानसिक अस्तित्व इन घटकों के ऊपर ही अवलम्बित रहता है। देखने में सभी का मस्तिष्क लगभग एक जैसा दीखेगा पर उसकी सूक्ष्म स्थिति में पृथ्वी, आकाश जैसा अन्तर दीखता है, उसके आधार पर व्यक्तित्वों का घटिया बढ़िया होना सहज ही आंका जा सकता है। यही सूक्ष्मता कुण्डलिनी के सम्बन्ध में व्यक्त की जा सकती है। मूलाधार, सहस्रार, ब्रह्म-नाड़ी, इड़ा, पिंगला उन्हें शल्य क्रिया द्वारा नहीं देखा जा सकता। यह सारी दिव्य रचना ऐसी सूक्ष्म है, जो देखी तो नहीं जा सकती पर उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है।
मूलाधार में अवस्थित कुण्डली महाशक्ति मलद्वार और जननेन्द्रिय के बीच लगभग चार अंगुल खाली जगह में विद्यमान बताई जाती है। योग शास्त्र के अनुसार इस स्थान पर वही गह्वर में एक त्रिकोण परमाणु पाया जाता है। यों सारे शरीर में स्थिति कण गोल बताये जाते हैं यही एक तिकोना कण है यहां एक प्रकार का शक्ति भ्रमर है। शरीर में प्रवाहित होने वाली तथा मशीनों से संचारित बिजली की गति का क्रम यह है कि वह आगे बढ़ती है फिर तनिक पीछे हटती है और उसी क्रम से आगे बढ़ती पीछे हटती हुई अपनी अभीष्ट दिशा में दौड़ती चली जाती है। किन्तु मूलाधार स्थिति त्रिकोण कण के शक्ति भंवर में सन्निहित बिजली गोल घेर में पेड़ से लिपटी हुई बेल की तरह घूमती हुई संचारित होती है। यह संयम क्रम प्रायः 3।। लपेटों का है। आगे चल कर यह विद्युत धारा इस विलक्षण गति को छोड़ कर सामान्य रीति से प्रवाहित होने लगती है।
यह प्रवाह निरन्तर मेरु दण्ड में होकर मस्तिष्क के उस मध्यबिन्दु तक दौड़ता रहता है, जिसे ब्रह्म-रन्ध्र या सहस्रार कमल कहते हैं। इस शक्ति केन्द्र का मध्य अणु भी शरीर के अन्य अणुओं से भिन्न रचना का है। वह गोल न होकर चपटा है। उसके किनारे चिकने न होकर खुरदरे हैं—आरी के दांतों से उस खुरदरेपन की तुलना की जा सकती है। योगियों का कहना है कि उन दांतों की संख्या एक हजार है। अलंकारिक दृष्टि से इसे एक एक कमल पुष्प की तरह चित्रित किया जाता है। जिसमें हजार पंखुरियां खिली हुई हों। इस अलंकार के आधार पर ही इस अणु का नामकरण ‘सहस्रार कमल’ किया गया है।
सहस्रार कमल का पौराणिक वर्णन बहुत ही मनोरम एवं सारगर्भित है। कहा गया है कि क्षीरसागर में विष्णु भगवान् सहस्र फन वाले शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। लक्ष्मी उनके पैर दबाती हैं। कुछ पार्षद उनके पास खड़े हैं। क्षीरसागर मस्तिष्क में भरा हुआ, भूरा चिकना पदार्थ ग्रेमैटर है। हजार फन वाला सर्प यह चपटा खुरदरा ब्रह्म-रन्ध्र स्थित विशेष परमाणु है। मनुष्य शरीर में अवस्थित ब्रह्म-सत्ता का केन्द्र यही है। इसी से यहां विष्णु भगवान का निवास बताया गया है। यह विष्णु सोते रहते हैं। अर्थात् सर्वसाधारण में होता तो ईश्वर का अंश समान रूप से है पर वह जागृत स्थिति में नहीं देखा जाता। आमतौर से लोग घृणित, हेय, पशु-प्रवृत्तियों जैसा निम्न-स्तर का जीवन यापन करते हैं। उसे देखते हुए लगता है कि इनके भीतर या तो ईश्वर है ही नहीं—अथवा यदि है तो वह प्रसुप्त स्थिति में पड़ा है। जिसका ईश्वर जागृत होगा उसकी विचारणा, क्रियाशीलता आकांक्षा एवं स्थिति उत्कृष्ट स्तर की दिखाई देगी वह प्रबुद्ध और प्रकाशवान् जीवन जी रहा है, अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशवान् न हो रहा होगा वरन् दूसरों को भी मार्ग-दर्शन कर सकने में समर्थ हो रहा होगा। मानव तत्त्व की विभूतियां जिसमें परिलक्षित न हो रहीं हैं, जो शोक-संताप, दैन्य दारिद्र और चिन्ता-निराशा का नारकीय जीवन जी रहा हो, उसके बारे में यह कैसे कहा जाय कि उसमें भगवान् विराजमान हैं। फिर यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें ईश्वर नहीं है। हर जीव ईश्वर का अंश है और उसके भीतर ब्रह्म सत्ता का अस्तित्व विद्यमान भी है।
इस विसंगति की संगति मिलाने के लिए यही कहा जा सकता है कि उसमें भगवान् है तो पर सोया पड़ा है। क्षीर जैसी उज्ज्वल विचारणाओं के सागर में भगवान् निवास करते हैं। क्षीर सागर ही उनका लोक है। जिस मस्तिष्क में क्षीर जैसी धवल स्वच्छ, उज्ज्वल प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां भरी पड़ी हों समझना चाहिए कि उसका अन्तरंग क्षीरसागर है और उसे भगवान् का लोक ही माना जायेगा। क्षीरसागर में सहस्र फन वाले शेषनाग पर विष्णु भगवान् के शयन करते रहने का यही पौराणिक रहस्य है।
विष्णु के हाथ चार आयुध। शंख अर्थात् ध्वनि, वाक् शक्ति, दूसरों को जगाने-उठाने एवं प्रभावित करने की क्षमता। चक्र अर्थात् गतिशीलता, क्रिया, स्थिति के अनुरूप परिवर्तन कर सकने की शक्ति। गदा अर्थात् प्रताड़ना, अवांछनीय, अनुपयुक्त परिस्थितियों को दबाने-मिटाने एवं सुधारने की सामर्थ्य। पद्म अर्थात् सौन्दर्य, शोभा; सुगन्ध, मधुरता, सौम्यता, सज्जनता सहृदयता, उदारता, संयमशीलता आदि सद्गुणों का बाहुल्य। विष्णु भगवान् के चार हाथों में यह चार आयुध हैं। भगवान् अपने साथ यह विशेषतायें धारण किये हैं। जिनका भगवान् जागृत, सक्रिय होगा, उनमें उपरोक्त चारों विशेषतायें भी प्रत्यक्ष परिलक्षित होंगी। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। जहां भगवान् रहेगा, वहां विभूतियां, सिद्धियां, विशेषतायें, सफलतायें, सद्भावनायें प्रचुर परिमाण में दृष्टिगोचर होंगी। लक्ष्मी अर्थात् विभूति। वह विष्णु की पत्नी है। महापुरुषों के पास महान् विभूतियां भी प्रस्तुत रहती हैं। दरिद्रता तो दुर्जनों के हिस्से आई है, सज्जन अपरिग्रही हो सकते हैं, दरिद्रता तो दुर्जनों के हिस्से आई है, सज्जन अपरिग्रही हो सकते हैं, यह उनकी स्वेच्छा, सुविधा एवं अभिरुचि है। वैसे कोई अभाव उनके ऊपर थोपा हुआ नहीं होता।
नारद हयग्रीव आदि दूसरे पार्षदों की उपस्थिति का आधार यह है कि विष्णु और लक्ष्मी के साथ-साथ अनेक दैवी शक्तियां भी सहायता के लिए उपस्थित रहती हैं। सात्विक शक्तियों के ज्ञान-विज्ञान और वर्चस्व के प्रतीक नारद माने जाते हैं और बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, वैभव, साहस एवं सकाम महत्ता के प्रतिनिधि हयग्रीव हैं। सतोगुण का बाहुल्य और रजोगुण का सान्निध्य सदा विष्णु और लक्ष्मी की उपस्थिति के साथ जुड़ा रहेगा। जो ईश्वर भक्त, आस्तिक एवं आत्मदर्शी है, उसे विष्णु लक्ष्मी, पार्षद, क्षीरसागर, शेषनाग जैसी दिव्य सत्ताओं को अपने अन्तरंग में प्रतिष्ठित देखने का अवसर मिलेगा। उसके प्रबुद्ध मस्तिष्क में उपरोक्त सारी विशेषतायें विद्यमान रहेंगी। उसका व्यक्तित्व प्रकाशमान अनुकरणीय एवं ऐतिहासिक चिर-स्मरणीय बनकर रहेगा। उसकी उत्कृष्ट विचारणा एवं आदर्श क्रियाशीलता उसे नर-पशु के स्तर से निकाल कर नर-नारायण की तरह पूजार्ह बनाकर रहेगी।
कुण्डलिनी के ऊर्ध्व मुख ब्रह्म-रन्ध्र स्थित सहस्रार कमल के आधार पर शेषशायी विष्णु की अलंकारिक गाथा का रहस्य बहुत गम्भीर है, उसमें बताया गया है कि ऊर्ध्व मुख सहस्रार कमल यदि जागृत हो सके तो व्यक्ति अपने भीतर विष्णु और उसके समस्त वैभव कलेवर को अपने साथ जुड़ा ,गुंथा देख सकता है और सिद्ध-पुरुषों की तरह महामहिम जीवन-यापन कर सकता है।
कुण्डलिनी के अधोमुख मूलाधार चक्र के साथ समुद्र-मन्थन की पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है। सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मथा था और एक से एक बढ़कर महत्त्वपूर्ण चौदह रत्न प्राप्त किये थे। इस गाथा में पौराणिक उपाख्यानकार ने कुण्डलिनी की गरिमा ही प्रकट की है।
सुर और असुर दो वर्ग माने गये हैं। इनकी प्रकृति भिन्न है। दिति-अदिति दो माताओं के पुत्र होने के कारण इनमें कुछ भेद भी है पर पिता एक होने के कारण वे एक ही अंश-वंश के तथा परस्पर पूरक हैं। सुर-गुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य दोनों ही देव थे। दोनों की योग्यता, तपस्या एवं दूरदर्शिता असाधारण थी। प्रक्रिया में थोड़ा अन्तर अवश्य था पर थे दोनों ही अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण। सुरु गुरु वृहस्पति ज्ञान मार्गी थी, उनका सम्प्रदाय योग को प्रधानता देता था और उनके अनुयायी दक्षिण मार्गी कहलाते थे। असुर गुरु शुक्राचार्य कर्ममार्गी थे; उनका सम्प्रदाय तन्त्र को प्रधानता देता था और उनके अनुयायी वाम-मार्गी कहलाते थे। आगम और निगम, वेद और तन्त्र दोनों की अपनी महत्ता है। ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सुर और असुरों की सत्ता एक दूसरे की पूरक हैं। पर समन्वय का पथ छोड़ने वाले एक ही पन्थ परिवार के लोग दुराग्रह के कारण टकराते रहते हैं, सो अतिवादिता और उग्र दुराग्रह का दौर जब चला तो सुर, असुर भी टकराने लगे। देवासुर संग्राम के बहुत कथानक पुराणों में पाये जाते हैं पर उनके सहयोग पूर्ण क्रियाकलापों का भी सर्वथा अभाव नहीं है। समुद्र-मन्थन दोनों ने मिलकर किया था। प्रजापति ने परस्पर कलह से उन्हें दिन-दिन दुर्बल होते जाते, देख कर परामर्श दिया कि वे सहयोग का महत्त्व समझें और मिल-जुलकर काम करें। उन्होंने परामर्श माना और समुद्र-मन्थन का पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो गये। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सुर-असुर सम्मिलन है। विष्णु को ज्ञान का और शिव को कर्म का प्रतीक माना गया है। सुरों का उपास्य विष्णु और असुरों का उपास्य शिव माना जाता रहा है। यह तथ्य कुण्डलिनी महाशक्ति के सुविस्तृत विज्ञान में बहुत ही स्पष्ट है।
मस्तिष्क के मध्य भाग में अवस्थित सहस्रार कमल में शेषशायी विष्णु भगवान अवस्थित हैं और अधःअवस्थित मूलाधार चक्र के अधिपति शिव हैं। शिव चरित्र में काम देव द्वारा शिव को उद्दीप्त करने और उनके द्वारा तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला डालने वाली कथा प्रख्यात है। कुण्डलिनी जननेन्द्रिय केन्द्र के समीप होने से अपने निकटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करती है, तत्त्वदर्शी उस अपव्यय को ज्ञान नेत्र खोलकर नियन्त्रित कर लेते हैं। एक पौराणिक कथा इसी सन्दर्भ में यह भी है कि शिव के काम पीड़ित होने पर उनकी जननेन्द्रिय के 18 टुकड़े विष्णु ने कर डाले और वे जहां भी गिरे वहां ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का उद्भव इसी प्रकार हुआ। वासना को ज्योति में बदला जा सकता है। इस कथानक का यही मर्म है।
शिवजी का प्रधान आभूषण सर्प है और उनके चित्रों में हर सर्प प्रायः 3।। फेरे लगाकर लिपटा हुआ दिखाई पड़ता है। शिवलिंग की मूर्ति पूजा में नर-नारी की जननेन्द्रियों की ही स्थापना है। शिव मन्दिरों की प्रतिमा में नर-नारी की जननेन्द्रियों को सम्मिलित करके प्रतिष्ठापित किया जाता है और उस पर जल चढ़ाने की—शीतल करने की प्रक्रिया जारी रहती है। अर्थात् इन अवयवों को यों अश्लील और गुह्य माना जाता है पर वे घृणित नहीं हैं। उनमें ऐश्वर्य के असाधारण रहस्य बीज विद्यमान् हैं। प्रतीक रूप से सर्प जलहली और शिवलिंग की पाषाण प्रतिमा के बीच भी अवस्थित रहता है। इस स्थापना में इसी तथ्य का प्रतिपादन है कि कुण्डलिनी का अधिपति शिव प्रत्यक्ष एवं समर्थ परमेश्वर है। उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत और मानसरोवर की तरह समझे जायें उन्हें नर-नारी की घृणित जननेन्द्रिय मात्र न मान लिया जाय। वरन् उनकी पवित्रता और महत्ता के प्रति अति उच्च भाव रखते हुए, सदुपयोग की आराधना में तत्पर रहा जाय। साहस और कलाकारिता के—पुरुषार्थ और लालित्य के—कर्म और भावना के इन केन्द्रों को प्रजनन मात्र से निरस्त न बना दिया जाय वरन् नर-नारी की जननेन्द्रियों के निकट मूलाधार चक्र की शिव शक्ति को उच्च आदर्शों के लिए प्रयुक्त किया जाय। भारतीय अध्यात्म-शास्त्र का यह संदेश हर किसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। शिवलिंग की प्रतिमाओं में इसी तथ्य का संकेत रूप में प्रकटीकरण है।
कृष्ण की रासलीला में गोपियों के साथ वेणुनाद और अनहद नृत्य में अलंकारिक रूप से अन्तरंग की समस्त भाव तरंगों को सरसता से ओत-प्रोत, झंकृत एवं उल्लसित करने का संकेत है। स्नान करती गोपियों के वस्त्र ले भागने और उन्हें नग्न करने में भी यही अलंकार है कि उस गुह्य शक्ति को तिरस्कृत, उपेक्षित एवं विस्मृत न रखकर उस पर पड़ा पर्दा हटाकर तथ्य को तात्त्विक दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिये। तांत्रिक साधनाओं में ‘भैरवी-चक्र’ की साधना असामाजिक एवं अश्लील होने के कारण उसकी चर्चा नहीं की जाती और उसे अति गुप्त रखा जाता है। रामकृष्ण परमहंस में अद्भुत शक्तियों का जागरण करने के लिए उनकी तांत्रिक गुरु महायोगिनी ने ‘कुमारी पूजा’ की साधना कराई थी। उसके अश्लील क्रिया-कलापों में सहयोग देने के लिए परमहंस जी की धर्मपत्नी शादरामणि जी बड़ी कठिनाई से ही अपनी सहज संकोचशीलता छोड़कर तैयार हुई थीं। आध्यात्मिकता का एक काम शास्त्र भी है। जिसके अनुसार कुन्ती द्वारा सर्वथा कुमारी होते हुए भी देव शक्तियों का आह्वान कर सूर्य का प्रसाद कर्ण, इन्द्र का प्रसाद अर्जुन, धर्मराज का प्रसाद युधिष्ठिर और वरुण का प्रसाद भीम उत्पन्न किया था। अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान के पिता मरुत थे, इसलिए उन्हें मारुत भी कहा जाता है। इस शास्त्र का एक सुविस्तृत विज्ञान है पर उसकी चर्चा केवल अधिकारी वर्ग तक ही सीमित रहने योग्य होने से उसका सार्वजनिक उल्लेख अवांछनीय समझा गया है। अस्तु तन्त्र की ऐसी ही अनेक प्रक्रियाओं को गुह्य घोषित करके उसे अधिकारी वर्ग के लिए ही सीमित और सुरक्षित कर दिया गया है।
कृष्ण चरित्र में कालिया नाग का मान मर्दन करने और उसकी दोनों पत्नियों द्वारा भगवान् की अनेक उपहारों सहित अभ्यर्थना करती हुई प्रस्तुत होने की कथा प्रसिद्ध है। कृष्ण, विष्णु के अवतार हैं। उद्धत महासर्प को वे ही नियन्त्रित करते हैं। हमारा मनःसंस्थान महासर्प है, यदि वह उद्धत हो जाय तो विष उगलता है और सर्वनाश का सरंजाम जुटाता है। पर यदि उसे नियन्त्रित कर लिया जाय तो उसकी दोनों पत्नी ऋद्धि और सिद्धि अगणित विभूतियों का उपहार साथ लेकर अभ्यर्थना के लिए उपस्थित होती हैं। कथा प्रसिद्ध है कि पृथ्वी का भार शेषनाग के शिर पर रखा है। उपरोक्त महासर्प ही जीवन धारण किये रहने का आधार है। प्राण के समस्त स्फुल्लिंग उसी के गह्वर में छिपे पड़े हैं। महाप्राण का अधिपति वही है।
समुद्र-मन्थन के प्रसंग में सुर-असुर का विवेचन ऊपर हो चुका है। ज्ञान कर्म का समन्वय देवासुर सहयोग है। सुमेरु पर्वत यह तिकोना परमाणु है, जिसके कारण मूलाधार चक्र की रचना हो सकी। प्रसिद्ध है कि सुमेरु पर्वत पर देवता रहते हैं और स्वर्ण का बना है। निस्सन्देह इस त्रिकोण में एक से एक अद्भुत दिव्य शक्तियों और स्वर्ण सम्पदाओं का समावेश है। सुमेरु की रई, शेषनाग की रस्सी बनाकर समुद्र मथा गया। यह सर्प रज्जु—ब्रह्म नाड़ी के अन्तर्गत इड़ा पिंगला की विद्युत धाराओं से ओत-प्रोत है। शिव और विष्णु के प्रतीक ज्ञान और कर्म सुर और असुर जब समुद्र-मन्थन की—कुण्डलिनी जागरण की महासाधना में संलग्न हुए तो उसे सफल बनाने में प्रजापति ब्रह्मा ने कूर्म बनकर उसका बोझ अपने ऊपर उठा लिया। प्रयत्न असफल न हो जाय—सुमेरु नीचे न धंसक जाय—इस आशंका को निरस्त करने के लिए कूर्म भगवान् ने अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत जैसा भार उठा लिया। साधना पथ के पथिकों का उत्तरदायित्व भगवान् वहन करते हैं और सफलता का पथ पुरुषार्थ एवं निष्ठा के अनुरूप निरन्तर प्रशस्त होता चला जाता है। प्रथम चरण में ही चौदह रत्न नहीं निकल आये वरन् उसके लिए देर तक निष्ठापूर्वक मन्थन की प्रक्रिया जारी रखनी पड़ी। आध्यात्मिक साधनाओं में उतावली करने वाले अधीर व्यक्ति सफल नहीं होते, उसका लाभ तो धैर्यवान और श्रद्धा को मजबूती के साथ पकड़े रहकर विश्वासपूर्वक निर्दिष्ट मार्ग पर अग्रसर होते रहने वाले साधक—नैष्ठिक साधक ही उठा पाते हैं।
समुद्र-मन्थन की साधना के फलस्वरूप चौदह रत्न उपलब्ध हुए थे—
(1) लक्ष्मी, (2) कौस्तुभ मणि, (3) पारिजात पुष्प, (4) वारुणी, (5) धन्वन्तरि, (6) चन्द्रमा, (7) कामधेनु, (8) ऐरावत हाथी, (9) रम्भा-नर्तकी, (10) उच्चैश्रवा अश्व, (11) अमृत, (12) धनुष, (13) शंख, (14) विष।
पौराणिक उपाख्यान के अनुसार उनमें से अधिकांश रत्न देवताओं को उपलब्ध हुए। दैवी प्रकृति के व्यक्ति ही अपनी सत्पात्रता के आधार पर दिव्य विभूतियों का सदुपयोग करके लाभान्वित हो पाते हैं। दुष्प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति उपलब्धियों को गंवा ही देते हैं और उन्हें प्रकृति के नियमानुसार खाली हाथ ही रहना पड़ता है।
लक्ष्मी अर्थात् सम्पन्नता। कौस्तुभ मणि (पारस) अर्थात् जो भी सम्पर्क में आये उसका महत्वपूर्ण बन जाना। परिजात अर्थात् पुष्प-सी कोमलता, शोभा, सुगन्ध और प्रसन्नता। वारुणी अर्थात् आदर्शों के प्रति उत्साह भरा उल्लास। धनवन्तरि अर्थात् आरोग्य दीर्घजीवन। चन्द्रमा अर्थात् शांति, शीलता। कामधेनु अर्थात् अवांछनीय कामनाओं की समाप्ति और उचित कामनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक श्रमशीलता का उद्भव। ऐरावत हाथी अर्थात् धैर्य-विवेक सहित बलिष्ठता। रम्भा अर्थात् कलात्मक सरसता, भावुकता एवं सौन्दर्य दृष्टि। उच्चेश्रवा अश्व अर्थात् अदम्य साहस और अथक पुरुषार्थ। अमृत अर्थात् आत्म-ज्ञान, आत्मा के स्वरूप और जीवनोद्देश्य की अनुभूति। धनुष अर्थात् अभीष्ट साधनों की उपलब्धि। शंख अर्थात् दूसरों को सजाना और प्रभावित कर सकने वाली प्रखर वाणी। इन तेरह विभूतियों के साथ-साथ एक जोखिम भी साथ ही जुड़ी हुई है कि यदि इन विभूतियों को पाकर व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाय और उनका दुरुपयोग करने लगे तो वे ही विष तुल्य अपने और दूसरों के लिए घातक परिणाम भी उत्पन्न कर सकती है।
रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर, वृत्तासुर आदि असुरों ने तपश्चर्या की कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अनेकों वरदान और वैभव प्राप्ति किये थे, किन्तु उद्धत मनोभूमि एवं निकृष्ट अन्तःस्तर होने के कारण उनने जो पाया वह खो ही न गया वरन् विष तुल्य सिद्ध होकर सर्वनाश का कारण बना। समुद्र-मन्थन का चौदहवां रत्न विष भी है। जिसे कोई शिव साधक ही पचा सकता है। भगवान् शंकर ने संसार की क्षति न होने देने के उद्देश्य से समुद्र मन्थन से निकले हुए विष को अपने कण्ठ में धारण कर लिया था। संसार में दोष दूषण का अंश भी बहुत है, उसे न तो पेट में भरना चाहिए और न मुख से कटु, कर्कश बोना चाहिए। जहां सुधार सम्भव है, वहां प्रयत्न किया जाय अन्यथा दुरित को न तो खाना ही उचित है, न उगलना ही उसे कण्ठ में धारण किये रहना चाहिए। शिव ने यही किया। अध्यात्म साधना के साधकों को यही करना चाहिये। इस मार्ग पर चलते हुए विभूतियों की जो अमृतमयी उपलब्धि होती है, वह विषाक्त न होने पावे इसका ध्यान रखना चाहिए।
कुण्डलिनी साधना समुद्र-मन्थन की तरह है। उससे उपरोक्त चौदह रत्न हर साधक को मिल सकते हैं। अधः और ऊर्ध्व ध्रुव केन्द्रों में वह सब कुछ भरा पड़ा है, जो संसार में कहीं भी विद्यमान है। सहस्रार और मूलाधार के रत्न भण्डारों की तिजोरी खोल सकने की चाबी का नाम ही कुण्डलिनी साधना है, जो उसे कर सकें, उन दुस्साहसियों को इस संसार का अति सौभाग्यशाली व्यक्ति बनने का अवसर मिलता है।