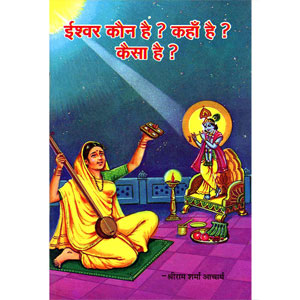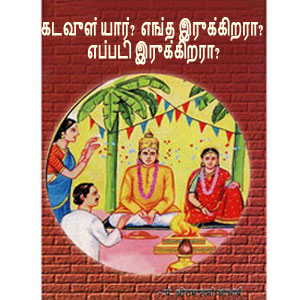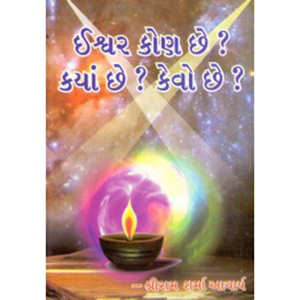ईश्वर कौन है कहाँ है कैसा है 
दयानिधान भगवान के महान् अनुदान
Read Scan Version
भगवान को दया निधान, करुणा सिन्धु, अजस्र दानी कहा गया है। उसका कितना अधिक अनुदान मनुष्य को मिला है उसे यदि समझा जा सके तो उस करुणा सागर की अनुकम्पा के प्रति हृदय कृतज्ञता से भर जाय और इसके लिए भावना उमड़े कि ऐसे उपकारी अभिभावक के अनुशासन में रहना, निर्देशित रीति-नीति का पालन करना ही उचित है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता सर्वविदित है। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के साथ-साथ उस पर यह उत्तरदायित्व भी आया कि भगवान की सृष्टि को सुन्दर, समुन्नत और सुरभित बनाने के लिए काम करे। और ईश्वर की उस इच्छा, आशा को पूरी करे जो मनुष्य को विशेष अनुदान देते समय उसने अपने मन में रखी थी।
भगवान मनुष्य के लिए ही नहीं अपने सभी पुत्रों के प्रति उदार है। प्रत्येक जीवन को उसने उनकी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप क्षमतायें और विशेषतायें दी हैं। यदि प्राणियों को शरीर ही मिले होते कुछ अतिरिक्त विशेषता न मिली होती तो उनका जीवन ही दुर्लभ हो जाता।
परमेश्वर की प्राणियों से सम्बन्धित शक्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं—अतिशय उदार है। उसने मुक्त हस्त से प्राणियों को बहुत कुछ दिया है। जीवन धारण करने और सुख-सुविधा के साथ जीने के लिए ही नहीं—आत्म रक्षा के लिए भी वे विशेषतायें दी हैं जिनके आधार पर वे आगत विपत्ति एवं कठिनाई का मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें।
किसी भी प्राणी पर दृष्टिपात करें उसे भी प्रकृति का प्यार, संरक्षण और अनुदान प्राप्त हुआ। ऐसा प्रत्यक्ष दीखता है। जन्मदात्री प्रकृति ‘कुमाता’ नहीं हो सकती उसका असीम स्नेह तो सब पर बरसता है। अन्य प्राणी उसका सदुपयोग करते हैं और दुर्बल, असमर्थ प्रतीत होते हुए भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर लेते हैं।
दक्षिणी अमेरिका में एक पक्षी पाया जाता है उसका नाम है ‘स्लाथ’ यह संसार के सबसे अधिक आलसी जीव के रूप में विख्यात है। अपना अधिकांश जीवन वह पेड़ पर उल्टा लटके-लटके ही काट देता है। अपने आस-पास की टहनियां और पत्ते ही उसका भोजन हैं। वर्षा ऋतु आती है पानी बरसता है किन्तु वह अपनी शीर्षासन मुद्रा का परित्याग नहीं करता। यह प्रकृति के ज्ञान और उसकी महान् कृपा का ही फल कहना चाहिये कि उसके रोयें सीधे न होकर उलटे बनाये गये हैं जिससे उसके शरीर पर आया सारा पानी टपक जाता है अन्यथा उसका नाम अब तक लुप्त प्रायः जीवों की सारिणी में आ गया होता।
ह्वेल मछली संसार का सबसे बड़ा जानवर है। बाइबिल में इसे ‘महामत्स्य’ लिखा गया है और सचमुच ही उसका मीलों लम्बा दैत्याकार इस सम्बोधन के सर्वथा अनुरूप है। जब वह सांस छोड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे से फौवारे छूट रहे हों। एक बार एटलांटिक महासागर में ह्वेल का शिकार किया गया। सांघातिक चोट खाये मत्स्यराज का पेट चीड़ा गया तो उसके पेट के भीतर से पूरे 6 फीट लम्बा और 4 फीट चौड़ा एक कटल मछली का टुकड़ा निकला। 18 फीट लम्बा एक अस्थि पिंजर जो तब तक पच नहीं सका था और शार्क मछली का था उसके पेट से निकला।
इतनी बड़ी मछली जो पचासों हाथियों को भी तौल सकती है समुद्र के सारे जीवों को साफ कर गई होती यदि प्रकृति ने उसका मुंह छोटा न बनाया होता। इसका जबड़ा इतना छोटा होता है कि हेटिंग नामक समुद्री मछली उसके गले में फंसकर श्वांस की गति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार प्रकृति अन्य समुद्री जीवों की रक्षा करती है।
उड़ने से लेकर मौसम के हर उतार-चढ़ावों को बर्दाश्त करने की जितनी क्षमता चिड़िया के पंखों में होती है वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रकृति की उस रचना के समकक्ष आज तक कोई भी आविष्कार मनुष्य नहीं कर सका।
दक्षिण अमेरिका का उत्तरी कार्डिलरा प्रदेश सूखा अनुपजाऊ पहाड़ी क्षेत्र है न तो कोई पैदावार, न दूध देने वाले पशुओं की व्यवस्था। वृक्ष भी सूखी पत्तियों वाले पाये जाते हैं। प्रकृति को ‘‘कुमाता भवति’’ मान लिया जाता यदि उसने इस सूखे प्रदेश में जीवन की रक्षा का प्रबन्ध न किया होता। दया दर्शायी उसने और यह एक पौधा पैदा किया—गोवृक्ष (काऊ ट्री)। देखने में इसकी शाखायें मृत और सूखी जान पड़ती हैं पर जब इसका तना कुरेदा जाता है तो उसमें एक प्रकार का दूध निकलता है जो मीठा और पौष्टिक ही नहीं होता वरन् अन्न और तरकारियों में पाये जाने वाले सारे तत्व भी उसमें पाये जाते हैं। प्रातःकाल भूख लगती है और प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही यह इतना दूध दे देता है कि वहां के नीग्रो दिन भर अपना काम चलाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस दूध की जांच की तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गये कि इस दूध और पशुओं द्वारा प्राप्त दूध में बहुत घनिष्ठ एकता है।
शायद प्रकृति को मालूम था कि सहारा जैसे रेगिस्तान में ऊंट को ही एक मात्र वाहन बनाना पड़ेगा। वहां मनुष्य को तो जल मिलता नहीं ऊंट को कौन पानी पिलायेगा उसकी चिन्ता उसने स्वतः की और उसको वह क्षमता प्रदान की जिससे वह एक बार में पूरे 90 लीटर तक पानी पी लेता है और उससे सप्ताहों तक कड़ी धूप में भी अपना गुजारा कर लेता है।
शेर यों तो किसी का भी शिकार कर डालता है किन्तु यदि उसे 5 मील की दूरी पर एक जिराफ दिखाई दे जाये पर इससे कम दूरी पर अन्य जानवर हो तो भी वह कितना भी परिश्रम करना पड़े जिराफ को ही मारने की कोशिश करता है। एक प्रकार का गुलाब जामुन है जिराफ शेर के लिए। फिर अब तक जिराफ की नस्ल बची क्यों है उत्तर वही फिर वही मिलेगा—प्रकृति की दया और ममता के कारण। उसने जिराफ की खाल ऐसी बनाई है कि वह पेड़ों के बीच खड़ा हो जाता है तो बहुत पास पहुंचकर भी उसे पहचानना कठिन हो जाता है। सांप—अच्छा हुआ कि प्रकृति ने उसे पृथ्वी के अन्दर छिपा रहने वाला जीव बनाया वरना एक सांप का जहर हजार व्यक्तियों को मार सकता है। जावा और मलेशिया में एक प्रकार के सर्प पाये जाते हैं जिनके पंख होते हैं और वह उड़ते भी हैं। वे अधिकांश एक पेड़ से दूसरे पर उड़ कर ही जाते हैं उड़ते समय वे चपेट हो जाते हैं और नीचे जमीन पर उतरते समय गोलाकार होते हुए उतरते हैं। इस प्रकार उन्हें आहार प्राप्त करने की, आत्मरक्षा की तथा क्रीड़ा-कल्लोल की विविध सुविधायें मिली हुई हैं। पहलवान पहले अपने घरेलू अखाड़ों में कुश्ती का अभ्यास करते हैं तब कहीं बाहरी दंगलों में दांव-पेंच दिखाने का साहस करते हैं। विदेशी सैनिकों से लड़ने के पहले देशी फौजें अपने आपको दो हिस्सों में बांटकर युद्ध का नकली अभ्यास करती हैं। ऐसा न किया जाये तो असली युद्ध लड़ना मुश्किल पड़ जाये। इस तरह का सूक्ष्म ज्ञान तक प्रकृति ने अपने नन्हें-नन्हें मनुष्येत्तर जीवों को प्रदान किया है।
घरों में पाई जाने वाली गौरैया जितनी सीधी और सरल होती है उतनी ही लड़ाकू। पर शत्रु से लड़ने के लिए जवांमर्दी, वह नकली युद्धाभ्यास करके पैदा करती है। उसकी यह नकली लड़ाइयां देखते ही बनती हैं ऐसे दायें बायें से आक्रमण और बचाव करती हैं मानो, वियतनाम और वियतकांग का गोरिल्ला युद्ध चल रहा हो।
नर भुनगा आक्रमण करने में कोई ज्यादा चतुर नहीं होता वह दुश्मन को हरा भी नहीं सकता फिर बेचारा अपनी जीवन रक्षा कैसे करता? उसे प्रकृति ने धमकाने और डरा कर शत्रु को भगाने की विद्या सिखाई कोई शत्रु आता है तो वह अपने जबड़े ऐसे फैलाता है मानो कच्चा ही निगल जायेगा। आक्रमणकारी डरकर भाग जाता है तो भुनगा मौज से दूसरी तरफ चल देता है। इसे प्रकृति का प्रशिक्षण न कहा जाये तो और क्या कहा जाये?
कार्बोलिक एसिड एक जहरीला रसायन है इसे खाकर कोई जिन्दा नहीं रह सकता। उसकी मात्रा अपने स्वाभाविक विकास दर से बढ़ती रहती तो सारा संसार विषमय हो जाता। फिर बात क्या है जो अभी तक पृथ्वी अमृतत्व से ओत-प्रोत है। प्रोफेसर पी.जी. ग्रे नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसकी शोध की तो पाया कि मिट्टी में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं और इस तरह वे धरती माता को विषाक्त होने से बचा लेते हैं ऐसे कीटाणु एक दो नहीं 200 के लगभग तो अब तक खोजे भी जा चुके हैं। एक यह नन्हें कीटाणु हैं जो सामान्य होते हुए भी असामान्य कार्य करते हैं—भगवान् शिव के समान। एक है इन्सान जो संसार का विष—मानवता पर छाये विषैले वातावरण को मिटाने के लिए एक इन्च भी आगे नहीं बढ़ता भगवान् द्वारा प्रदत्त अपनी असामान्यता को कलंकित करता है। प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं का मनुष्य ने यदि सदुपयोग किया होता तो निस्सन्देह यह धरती तथाकथित स्वर्ग से कम नहीं वरन् अधिक ही साधन-सुविधाओं और सुख-शान्ति की प्रचुरताओं से भरी पूरी दीखती। इच्छा मात्र से अभीष्ट उपलब्धि
प्राणियों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं उनकी शारीरिक, मानसिक शक्तियों तथा भौतिक परिस्थितियों का सृजन करती हैं इस तथ्य को थोड़ा अधिक गहराई से विचार करने पर सहज ही जाना जा सकता है और उसके अनेकों प्रमाण पाये जा सकते हैं।
समझा जाता था कि वर्षा होने से वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, पर पाया यह गया है कि वृक्षों की आवश्यकता उधर उड़ने वाले बादलों को पकड़ कर घसीट लाती हैं और उसे अपने क्षेत्र पर बरसाने के लिए उन्हें बाध्य करती हैं। कुछ दिन पूर्व जहां बड़े रेगिस्तान थे पानी नहीं बरसता था और बादल उधर से सूखे ही उड़ जाते थे, पर अब जब वहां वन लगा दिये गये हैं तो प्रकृति का पुराना क्रम बदल गया और अनायास ही वर्षा होने लगी है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में अब यह नया सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि वहां की वन सम्पदा बादलों पर बरसने के लिए दबाव डालती है। बादलों की तुलना में चेतना का अंश वृक्षों से अधिक है इसलिए वे विस्तार में बादलों से कम होते हुए भी सामर्थ्य में अधिक हैं। अतएव दोनों की खींचतान में चेतना का प्रतिनिधि वृक्ष ही भारी पड़ता है।
आत्म-रक्षा प्राणियों की एक महती आवश्यकता है। जीवों में जागरुकता और पराक्रम वृत्ति को जीवन्त बनाये रखने के लिए प्रकृति ने शत्रु पक्ष का निर्माण किया है। यदि सभी जीवों को शान्तिपूर्वक और सुरक्षित रहने की सुविधा न मिली होती तो फिर वे आलसी और प्रमादी होते चले जाते। उनमें जो स्फूर्ति और कुशलता पाई जाती है वे या तो विकसित ही न होती या फिर जल्दी ही समाप्त हो जातीं।
सिंह, व्याघ्र, सुअर, हाथी, मगर आदि विशालकाय जन्तु अपने पैने दांतों से आत्म-रक्षा करते हैं और उनकी सहायता से आहार भी प्राप्त करते हैं। सांप, बिच्छू, बर्रे, ततैया, मधुमक्खी आदि अपने डंक चुभो कर शत्रु को परास्त करते हैं। घोंघा, केंचुआ आदि के शरीर से जो दुर्गन्ध निकलती है उससे शत्रुओं की नाक बंद करके भागना पड़ता है। गेंडा, कछुआ, सीपी, घोंघा, शंख, आर्मेडिलो आदि की त्वचा पर जो कठोर कवच चढ़ा रहता है उससे उनकी बचत होती है। टिड्डे का घास का रंग, तितली फूलों का रंग, चीते पेड़-पत्तों की छाया जैसा चितकबरापन गिरगिट मौसमी परिवर्तन के अनुरूप अपना रंग बदलता है। ध्रुवीय भालू बर्फ जैसा श्वेत रंग अपनाकर समीपवर्ती वातावरण में अपने को आसानी से छिपा लेते हैं और शत्रु की पकड़ में नहीं आते। कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, कूड़ा-करकट आदि के रंग में अपने को रंग कर कितने ही प्राणी आत्म-रक्षा करते हैं। शार्क मछली बिजली के करेन्ट जैसा झटका मारने के लिए प्रसिद्ध है। कई प्राणियों की बनावट एवं मुद्रा ही ऐसी भयंकर होती है कि उसे देखकर शत्रु को बहुत समझ-बूझकर ही हमला करना पड़ता है।
शिकारी जानवरों को अधिक पराक्रम करना पड़ता है इस दृष्टि से उन्हें दांत, नाखून, पंजे ही असाधारण रूप से मजबूत नहीं मिले वरन् पूंछ तक की अपनी विशेषता है। यह अनुदान उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर प्रकृति से प्राप्त किये हैं।
शेर का वजन अधिक से अधिक 400 पौंड होता है जबकि गाय का वजन उससे दूना होता है। फिर भी शेर पूंछ के सन्तुलन से उसे मुंह में दबाये हुए 12 फुट ऊंची बाड़ को मजे में फांद जाता है।
प्राणियों की शरीर रचना और बुद्धि संस्थान भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता है संकल्प शक्ति, इच्छा तथा आवश्यकता। यह सम्वेदनाएं जिस प्राणी की जितनी तीव्र हैं वे उतने ही बड़े अनुदान प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को जो विभूतियां उपलब्ध हैं उनका कारण उसकी बढ़ी हुई संकल्प शक्ति ही मानी गई है।
प्रकृति परायण वृक्ष
प्रकृति ने कुछ कायदे कानून ऐसे बनाये हैं जो सृष्टि सन्तुलन की दृष्टि से नितान्त आवश्यक हैं। इन नियमों को न केवल मनुष्यों के लिए वरन् अन्य प्राणियों के लिए भी बनाया गया है। यहां तक कि वनस्पतियों के लिए भी।
मनुष्यों में बुद्धि धन, बल, प्रतिभा, भावना आदि की सम्पदाएं ऐसी हैं जिन्हें उसके व्यक्तित्व का बीज कहा जा सकता है। इसी के आधार पर हम ऊंचे उठते और आगे बढ़ते हैं। बीज सड़ा-गला हो तो उससे वंश वृद्धि न हो सकेगी। गुण, कर्म, स्वभाव की विभूतियां यदि स्वस्थ और समर्थ न हों तो कोई व्यक्ति प्रगति के पथ पर दूर तक अग्रसर न हो सकेगा। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि हमारी विभिन्न शारीरिक और मानसिक हलचलें इन बीज तत्वों को विकसित, परिष्कृत और पुष्ट करने के लिए ही होती हैं। भौतिक और आत्मिक सम्पदाओं से अधिकाधिक मावा में सम्पन्न होने की अभिलाषा स्वाभाविक मानी जाती है—वह बनी ही रहती है—और उनके लिए जाने अनजाने प्रयास चलते ही रहते हैं।
वनस्पति-जगत में भी यही प्रक्रिया अपने ढंग से उसी तरह पलती रहती है जिस तरह मनुष्यों में चलती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्म-विस्तार है। हम बड़े, विकसित हों और सुदूर क्षेत्र तक फैलें इसके लिए भांति-भांति के प्रयत्न पुरुषार्थ किये जाते हैं यहां तक कि युद्ध भी। आध्यात्मिक क्षेत्र में यही विस्तार वार आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ाकर सबमें अपने को और अपने में सबको देखने वाला तत्व दर्शन हृदयंगम किया जाता है। बीज तत्व का विकास और सत्ता का विस्तार करने के लिये हम मनुष्यों के विभिन्न क्रिया-कलापों को संजोया जाना देखते हैं। यदि यह दो प्रवृत्तियां न होतीं तो कदाचित पेट और प्रजनन जैसी निकृष्ट स्तर के जीवों में पाई जाने वाली तुच्छ हलचलों के अतिरिक्त हम और कुछ महत्वपूर्ण सोचने या करने में समर्थ ही न हो पाते। ठीक यही बात वनस्पति-जगत पर भी लागू होती है।
पौधे बढ़ते और विकसित होते हैं। अन्ततः उनकी प्रौढ़ता फलवती होती है और उन पर फल लगते लदते हैं। यह फल मनुष्यों सहित अन्य प्राणियों के लिये आहार का काम देते हैं पर जहां तक वृक्ष के लिए इन फलों का अपना उपयोग है वह उनकी बीज सत्ता को अक्षुण्ण रखने, परिपुष्ट बनाने और सुविस्तृत करने के उद्देश्य में ही सन्निहित देखी जा सकती है। वृक्ष मात्र परोपकार के लिए ही नहीं फलते, उनके अपने जीवन की सार्थकता भी फलवान होने में ही हैं।
फलों में गूदा भरा होता है और गूदे के भीतर बीज रहते हैं। यह बीज एक जगह इकट्ठे नहीं रखे रहते वरन् दूर-दूर तक फासले पर रहते हैं। पूरे वृक्ष पर एक ही फल नहीं लगता वरन् उनकी बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था क्यों की इस पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि प्रगति के आधार जिस प्रकार मनुष्य के लिए बनाये गये हैं, वैसे ही वृक्षों के लिए भी विनिर्मित किये गये हैं।
गूदे का उद्देश्य है—बीज को पोषण देना, परिपुष्ट करना, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचना। माता के गर्भ में जिस प्रकार भ्रूण पकता, पलता है उसी प्रकार फल के उदर में गूदे के मध्य बैठा हुआ बीज धीरे-धीरे सबल और समर्थ बनता रहता है। मानव जीवन के अधिक तर क्रिया-कलाप भौतिक उपार्जन के लिये होते हैं। इससे सुविधा सामग्री तो मिलती ही है साथ ही वे विशेषतायें, विभूतियां भी परिपक्व होती हैं जिनके आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में सफलतायें पाई जा सकती हैं—जिन्हें विकसित व्यक्तित्व की परिपुष्ट सत्ता कहते हैं।
एक वृक्ष अनेक फल और प्रत्येक फल में अनेक बीज इसलिये उत्पन्न करता है कि उसकी सत्ता को अधिकाधिक विस्तार करने का अवसर मिले। उसे सीमित दायरे में संकीर्णता की परिधि में ही आबद्ध रहकर अविकसित कहलाने का कलंक न सहना पड़े। आत्मविस्तार बिना न तो आत्म-सन्तोष मिल सकता है और न आत्मगौरव। जब मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर—क्षुद्रता से महानता की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है तो वृक्ष भी उसी प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण क्यों न करें।
प्रत्येक बीज में एक पूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। परिपुष्ट होने के पश्चात् उसका अगला उद्देश्य वह रहता है कि उसी जाति के नये वृक्ष उत्पन्न करे। साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र की दृष्टि से समीपवर्ती सीमा बन्धन को लांघकर सुदूर क्षेत्रों तक अपनी सत्ता को सुविस्तृत बनाया जाय। फल के भीतर सारे बीज एक जगह ही इकट्ठे चिपके नहीं रहते। गूदे के भीतर वे थोड़ा-थोड़ा फासला देकर अलग-अलग जमे होते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि उन्हें पृथक्-पृथक् रूप से सुदूर क्षेत्र में जाने का और सुविस्तृत परिधि में विस्तार का अवसर मिले। यदि गूदे में सब बीज इकट्ठे रखे होते तो फल के पककर गिरने पर वे सभी एक जगह ही उगते। फलतः वे सभी एक दूसरे की खुराक छीनते—फैलने की जगह प्राप्त न कर पाते और ऐसे ही सूख मुरझाकर समाप्त हो आते। विस्तार के लिये यह आवश्यक है कि पुरखों के घर आंगन को छोड़कर अन्यत्र भी जाने और फैलने का प्रयत्न किया जाय।
वृक्ष की सत्ता फलों के माध्यम से यही सब करती रहती है। फलने और पकने के साथ-साथ उनकी वितरण चेष्टा भी उत्साहपूर्वक चलती है। गूदे में बीजों का स्थान अलग-अलग था भी इसीलिये कि उनके वितरण की व्यवस्था बन सके। आहार में प्रायः गूदा ही काम आता है। बीज कड़े होते हैं इसलिये वे फेंक दिये जाते हैं या संग्रह कर लिये जाते हैं। गूदा समाप्त हो जाने पर भी बीजों का अस्तित्व बना रहता है। यदि उन्हें पीसकर नहीं खाया गया है तो चबाने पर भी उनमें से अधिकांश साबुत बच जाते हैं। पेट में भी कम ही पचते हैं। मल मार्ग से निकल कर वे पृथ्वी पर बिखर जाते हैं और इधर-उधर छितराते धक्के खाते और वृद्धि करते हैं।
मनुष्य जीवन की प्रगति के भी दो आधार हैं एक भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हुए अपने में गुण, कर्म, स्वभावपरक बीज सत्ता को परिपुष्ट करना और दूसरा उस पुष्ट सत्ता को सुविस्तृत क्षेत्र में वितरण करके उन विभूतियों को दूर-दूर तक बिखेरना-विकसित करना। प्रथम चरण को शक्ति संचय कह सकते हैं और दूसरे चरण को सेवा साधना। बल-वृद्धि का, सामर्थ्य सम्पादन का उद्देश्य यही हो सकता है कि उनके वितरण विस्तार का लाभ सुदूर क्षेत्रों को मिले। जो लोग शरीर या परिवार के भीतर ही अपनी प्रतिभा का लाभ सीमित किये बैठे रहते हैं उन्हें गूदे के भीतर ही पहुंचाने वाले बीज की उपमा दी जाती है।
गूदे में पककर विकसित हुए बीज सुदूर क्षेत्रों तक फैले इसके लिये प्रकृति ने अनेकों प्रकार की व्यवस्थायें की हैं। प्राणियों द्वारा उनका खाया जाना और मल विसर्जन के साथ उनका दूर-दूर जा पहुंचना प्रत्यक्ष ही है। कई बीज फेंके या संग्रह करने पर किसी न किसी प्रकार वंश वृद्धि करने का अवसर पाने में सफल हो जाते हैं। बीजों का व्यवसाय भी होता है। अनाज की तरह अन्य बीज भी खरीदे-बेचे जाते हैं और वे यहां से वहां की यात्रा करते हैं। यह तो प्रचलित व्यवस्था हुई प्रकृति भी इस दिशा में भारी योगदान करती है और तरह-तरह के ऐसे साधन जुटाती है जिससे वह उत्पन्न हुई बीज सम्पदा किसी एक स्थान तक सीमित होकर न रह जाय वरन् उसे सुदूर क्षेत्रों में वितरित होने का अवसर मिले।
हवा असंख्यों बीजों को अपने साथ उड़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाती है। इस स्तर के हलके बीजों की वनस्पति जगत में कमी नहीं है। ‘कुनैन’ जिस सिनकोना पौधे से बनती है उस के बीज इतने हलके होते हैं कि एक औंस में 70 हजार तोले जा सकें। आर्किडो के बीज इससे भी हलके होते हैं। इनकी बनावट भी ऐसी होती है जैसे पक्षी के परों की। हलकापन और बनावट की विशेषता दोनों के कारण हवा उन्हें आसानी से उड़ा ले जाती है और कहीं से कहीं ले जाकर पटकती है। कुछ बड़े और भारी बीजों में सूर्यमुखी, डोंडिलिओन, सौक्स, बेलकुन, आक, सेंगर, सरकंडा आदि के बीज ऐसे हैं जो पैराशूट की तरह बने होते हैं वे हवा का तनिक-सा सहारा पाकर लम्बी उड़ान उड़ते हैं। नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। आक के बीज में जो रूई चिपकी होती है उससे उनका उड़ना कितना सुहावना लगता है। ब्लड फ्लावर, करची, न्यूमोनशिया, चाटियम जैसे पौधों के बीज भी रोएंदार होते हैं, जिनके कारण उनकी वायु यात्रा बड़ी सरल बन जाती है। अरलू, पराल, जरुल, सहजन, चीड़ के बीजों की बनावट भी पक्षियों के परों जैसी होती है। वे इच्छा से नहीं उड़ पाते पर हवा उनकी उड़ने की सारी व्यवस्था स्वयं जुटा देती है। कुछ तो पूरे फल ही उड़नशील होते हैं वे अपने बीज परिवार को लेकर क्षेत्र विस्तार का प्रयोजन पूरा करने के लिए हवा की सहायता से यात्रा करने पर उतर पड़ते हैं। ऐसे उड़ाक फलों में होलोक, मधुलता, जिमीकन्द, फ्रेक्सीनस, होपियामेपल, डिपटीरोकारपस, साल आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन में एलेथस की बनावट हवाई जहाज से बिलकुल मिलती-जुलती है, उसे देखकर यह असमंजस पड़ता है कि इन्हें देखकर हवाईजहाज बने या हवाईजहाज देखकर प्रकृति ने इन्हें बनाया है आंधियां-धूल, तिनके ही नहीं हल्के बीजों को भी अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और कहीं से कहीं उन्हें जा पटकती हैं, जड़ी-बूटियां प्रायः इसी प्रकार यहां से वहां जा पहुंचती हैं।
कुछ फल भी स्वार्थी मनुष्यों की तरह बड़े कृपण होते हैं। वे पके हुए बीजों को भी अपने सूखे खोखले में समेटे बैठे रहते हैं। स्वयं भले ही उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न हो पर दूसरों को लाभ न मिलने पाये, ऐसी मनोवृत्ति वाले मनुष्य ही नहीं फल भी दुनियां में मौजूद हैं। लाल पोस्त, सत्यानाशी, कुत्ताफूल, हंसलता तथा धतूरा इसी प्रकार के फल हैं। हवा जब इन्हें झकझोरती है तो खुद भी उलटने-पुलटने लगते हैं और बीजों को छोड़ने के लिये भी विवश होते हैं। स्वेच्छा से न सही बलात्कार से सही चलना उन्हें भी प्रकृति के कानूनों पर ही पड़ता है। संग्रही कोई बनना भी चाहे तो प्रकृति उसे वैसा करने की आज्ञा नहीं दे सकती। जो दिया गया है वह देने के लिये है जो यह नहीं जानते उन्हें इन फलों की तरह दुर्गति और बल प्रयोग का सामना करना पड़ता है।
पानी में उगने वाली वनस्पतियों के बीजों को लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। यह बीज हलके और हवा भरे स्पंज की तरह होते हैं, जिससे वे लहरों पर आसानी से तैरते रह सकें। नदियों और समुद्रों के तटों पर उगे हुए पेड़-पौधे भी अपने बीज, जल को समर्पित करके उन्हें अन्यत्र चले जाने की खुशी-खुशी छूट देते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो स्वजनों को अन्यत्र उपयोगी स्थानों पर जाने से रोककर घर की चहार-दीवारी में ही बन्द रखने के लिये मोहग्रस्त बना रहता है। कमल गट्ठे अक्सर पानी में तैरते हुए ही कहीं से कहीं जा सकते हैं। नारियल के फलों का पानी में गिरना और सहस्रों मील जन शून्य द्वीपों में जा उगना इसी प्रकार सम्भव हुआ है।
कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं। पक जाने और सूख जाने पर कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं। पक जाने और सूख जाने पर भी वे बीजों को बाहर नहीं निकलने देते। इस कठोर नियन्त्रण की उग्र प्रतिक्रिया होती है। बीज विद्रोह कर बैठते हैं और उस भीतरी तनाव से छिलका एक विस्फोट की तरह फटता है और बीज उछलकर बाहर निकल जाते हैं। गुलमेंहदी, बुलसेरिल, नाइटजेसमिल, अरण्ड, कालमेघ, वज्रदन्ती, फ्लाक्स, कंचनलता आदि फलों में अक्सर फटने और बीज उछलने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। प्रहलाद, विभीषण, कैकेयी, बालि आदि को अपने अभिभावकों एवं गुरुजनों के विरुद्ध इसी प्रकार विद्रोह करना पड़ा था। अनुचित प्रतिबन्ध के अहंकारी दुराग्रह अक्सर ऐसे ही विस्फोट उत्पन्न करते रहते हैं।
कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हवा, पानी, मनुष्य आदि की सहायता न पाने पर स्वयं ही अपनी प्रवृत्ति प्रेरणा से आत्म विस्तार का रास्ता अपने बलबूते बनाते हैं और जिसका भी अंचल हाथ लगे उसी को पकड़कर आगे चल पड़ते हैं। लटजीरा, गोखरू, वनऔखरा, चोर-कांटा, बुइया, ठोकरी, चित्रक आदि के फल अथवा बीज अपने कांटों के साथ पशु-पक्षियों के शरीरों एवं मनुष्यों के कपड़ों को पकड़ लेते हैं और उन पर सवारी गांठकर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं।
चींटियों, चूहे, गिलहरी आदि संग्रही प्रकृति के प्राणी बीजों को इकट्ठा करते हैं। बिलों में से छितरा कर वे फिर जहां-तहां जा पहुंचते हैं। पक्षियों के पैरों में चिपकी मिट्टी के साथ अथवा उनकी बीट के माध्यम से भी अनेक वनस्पतियां तथा वृक्ष लम्बी यात्रायें करते हुए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पहुंचते हैं।
वनस्पतियों और वृक्षों की यह आत्म-विस्तार की अपनी उपलब्धियों की सुदूर क्षेत्र में वितरण करने की प्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार पाई जाती है जैसी कि प्रकृति प्रेरणा मनुष्य को उपलब्ध है जो जीवन विद्या का मर्म जानते हैं वे अपनी आन्तरिक विशेषताओं को बीज सत्ता की तरह परिपक्व करने के लिए अपनी हलचलों का गूदा संजोये, साथ यह भी ध्यान रखें कि समस्त उपार्जन वितरण के लिए है ताकि संसार की शोभा-सुषमा का विस्तार होता रहे उसमें कमी न आने पाये।
इस प्रकृति प्रेरणा को ही ईश्वरीय विधान, उसकी विधि व्यवस्था धर्म या अध्यात्म कहा जा सकता है जो जिस सीमा तक इन प्रेरणाओं को हृदयंगम करने में सफल होते हैं उन्हें स्वयं सम्पन्न होती रहने वाली त्याग प्रक्रिया के अनुसार उसका लाभ सत्परिणाम के रूप में प्राप्त होता रहता है। इसी आधार पर कर्मफल की दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है। अच्छे कार्यों का, परमार्थिक प्रयासों का परिणाम सुखद आनन्ददायक होता है तो बुरे कार्यों, संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित प्रयासों का परिणाम भी दुखद व क्लेशदायी ही होता है, व्यक्तिवाद की संकीर्ण स्वार्थपरता को निरस्त करके लोकहित की जन कल्याण की सत्प्रवृत्तियों में अपनी विभूतियों को समर्पित करने की जीवन पद्धति का नाम ही मानवी संस्कृति है। इसके साथ यह भी समझने और विचार करने योग्य है कि परमात्मा की यह कारुणिक विधि-व्यवस्था सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगलमय है। उससे लाभ उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिये।
भगवान मनुष्य के लिए ही नहीं अपने सभी पुत्रों के प्रति उदार है। प्रत्येक जीवन को उसने उनकी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप क्षमतायें और विशेषतायें दी हैं। यदि प्राणियों को शरीर ही मिले होते कुछ अतिरिक्त विशेषता न मिली होती तो उनका जीवन ही दुर्लभ हो जाता।
परमेश्वर की प्राणियों से सम्बन्धित शक्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं—अतिशय उदार है। उसने मुक्त हस्त से प्राणियों को बहुत कुछ दिया है। जीवन धारण करने और सुख-सुविधा के साथ जीने के लिए ही नहीं—आत्म रक्षा के लिए भी वे विशेषतायें दी हैं जिनके आधार पर वे आगत विपत्ति एवं कठिनाई का मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें।
किसी भी प्राणी पर दृष्टिपात करें उसे भी प्रकृति का प्यार, संरक्षण और अनुदान प्राप्त हुआ। ऐसा प्रत्यक्ष दीखता है। जन्मदात्री प्रकृति ‘कुमाता’ नहीं हो सकती उसका असीम स्नेह तो सब पर बरसता है। अन्य प्राणी उसका सदुपयोग करते हैं और दुर्बल, असमर्थ प्रतीत होते हुए भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर लेते हैं।
दक्षिणी अमेरिका में एक पक्षी पाया जाता है उसका नाम है ‘स्लाथ’ यह संसार के सबसे अधिक आलसी जीव के रूप में विख्यात है। अपना अधिकांश जीवन वह पेड़ पर उल्टा लटके-लटके ही काट देता है। अपने आस-पास की टहनियां और पत्ते ही उसका भोजन हैं। वर्षा ऋतु आती है पानी बरसता है किन्तु वह अपनी शीर्षासन मुद्रा का परित्याग नहीं करता। यह प्रकृति के ज्ञान और उसकी महान् कृपा का ही फल कहना चाहिये कि उसके रोयें सीधे न होकर उलटे बनाये गये हैं जिससे उसके शरीर पर आया सारा पानी टपक जाता है अन्यथा उसका नाम अब तक लुप्त प्रायः जीवों की सारिणी में आ गया होता।
ह्वेल मछली संसार का सबसे बड़ा जानवर है। बाइबिल में इसे ‘महामत्स्य’ लिखा गया है और सचमुच ही उसका मीलों लम्बा दैत्याकार इस सम्बोधन के सर्वथा अनुरूप है। जब वह सांस छोड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे से फौवारे छूट रहे हों। एक बार एटलांटिक महासागर में ह्वेल का शिकार किया गया। सांघातिक चोट खाये मत्स्यराज का पेट चीड़ा गया तो उसके पेट के भीतर से पूरे 6 फीट लम्बा और 4 फीट चौड़ा एक कटल मछली का टुकड़ा निकला। 18 फीट लम्बा एक अस्थि पिंजर जो तब तक पच नहीं सका था और शार्क मछली का था उसके पेट से निकला।
इतनी बड़ी मछली जो पचासों हाथियों को भी तौल सकती है समुद्र के सारे जीवों को साफ कर गई होती यदि प्रकृति ने उसका मुंह छोटा न बनाया होता। इसका जबड़ा इतना छोटा होता है कि हेटिंग नामक समुद्री मछली उसके गले में फंसकर श्वांस की गति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार प्रकृति अन्य समुद्री जीवों की रक्षा करती है।
उड़ने से लेकर मौसम के हर उतार-चढ़ावों को बर्दाश्त करने की जितनी क्षमता चिड़िया के पंखों में होती है वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रकृति की उस रचना के समकक्ष आज तक कोई भी आविष्कार मनुष्य नहीं कर सका।
दक्षिण अमेरिका का उत्तरी कार्डिलरा प्रदेश सूखा अनुपजाऊ पहाड़ी क्षेत्र है न तो कोई पैदावार, न दूध देने वाले पशुओं की व्यवस्था। वृक्ष भी सूखी पत्तियों वाले पाये जाते हैं। प्रकृति को ‘‘कुमाता भवति’’ मान लिया जाता यदि उसने इस सूखे प्रदेश में जीवन की रक्षा का प्रबन्ध न किया होता। दया दर्शायी उसने और यह एक पौधा पैदा किया—गोवृक्ष (काऊ ट्री)। देखने में इसकी शाखायें मृत और सूखी जान पड़ती हैं पर जब इसका तना कुरेदा जाता है तो उसमें एक प्रकार का दूध निकलता है जो मीठा और पौष्टिक ही नहीं होता वरन् अन्न और तरकारियों में पाये जाने वाले सारे तत्व भी उसमें पाये जाते हैं। प्रातःकाल भूख लगती है और प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही यह इतना दूध दे देता है कि वहां के नीग्रो दिन भर अपना काम चलाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस दूध की जांच की तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गये कि इस दूध और पशुओं द्वारा प्राप्त दूध में बहुत घनिष्ठ एकता है।
शायद प्रकृति को मालूम था कि सहारा जैसे रेगिस्तान में ऊंट को ही एक मात्र वाहन बनाना पड़ेगा। वहां मनुष्य को तो जल मिलता नहीं ऊंट को कौन पानी पिलायेगा उसकी चिन्ता उसने स्वतः की और उसको वह क्षमता प्रदान की जिससे वह एक बार में पूरे 90 लीटर तक पानी पी लेता है और उससे सप्ताहों तक कड़ी धूप में भी अपना गुजारा कर लेता है।
शेर यों तो किसी का भी शिकार कर डालता है किन्तु यदि उसे 5 मील की दूरी पर एक जिराफ दिखाई दे जाये पर इससे कम दूरी पर अन्य जानवर हो तो भी वह कितना भी परिश्रम करना पड़े जिराफ को ही मारने की कोशिश करता है। एक प्रकार का गुलाब जामुन है जिराफ शेर के लिए। फिर अब तक जिराफ की नस्ल बची क्यों है उत्तर वही फिर वही मिलेगा—प्रकृति की दया और ममता के कारण। उसने जिराफ की खाल ऐसी बनाई है कि वह पेड़ों के बीच खड़ा हो जाता है तो बहुत पास पहुंचकर भी उसे पहचानना कठिन हो जाता है। सांप—अच्छा हुआ कि प्रकृति ने उसे पृथ्वी के अन्दर छिपा रहने वाला जीव बनाया वरना एक सांप का जहर हजार व्यक्तियों को मार सकता है। जावा और मलेशिया में एक प्रकार के सर्प पाये जाते हैं जिनके पंख होते हैं और वह उड़ते भी हैं। वे अधिकांश एक पेड़ से दूसरे पर उड़ कर ही जाते हैं उड़ते समय वे चपेट हो जाते हैं और नीचे जमीन पर उतरते समय गोलाकार होते हुए उतरते हैं। इस प्रकार उन्हें आहार प्राप्त करने की, आत्मरक्षा की तथा क्रीड़ा-कल्लोल की विविध सुविधायें मिली हुई हैं। पहलवान पहले अपने घरेलू अखाड़ों में कुश्ती का अभ्यास करते हैं तब कहीं बाहरी दंगलों में दांव-पेंच दिखाने का साहस करते हैं। विदेशी सैनिकों से लड़ने के पहले देशी फौजें अपने आपको दो हिस्सों में बांटकर युद्ध का नकली अभ्यास करती हैं। ऐसा न किया जाये तो असली युद्ध लड़ना मुश्किल पड़ जाये। इस तरह का सूक्ष्म ज्ञान तक प्रकृति ने अपने नन्हें-नन्हें मनुष्येत्तर जीवों को प्रदान किया है।
घरों में पाई जाने वाली गौरैया जितनी सीधी और सरल होती है उतनी ही लड़ाकू। पर शत्रु से लड़ने के लिए जवांमर्दी, वह नकली युद्धाभ्यास करके पैदा करती है। उसकी यह नकली लड़ाइयां देखते ही बनती हैं ऐसे दायें बायें से आक्रमण और बचाव करती हैं मानो, वियतनाम और वियतकांग का गोरिल्ला युद्ध चल रहा हो।
नर भुनगा आक्रमण करने में कोई ज्यादा चतुर नहीं होता वह दुश्मन को हरा भी नहीं सकता फिर बेचारा अपनी जीवन रक्षा कैसे करता? उसे प्रकृति ने धमकाने और डरा कर शत्रु को भगाने की विद्या सिखाई कोई शत्रु आता है तो वह अपने जबड़े ऐसे फैलाता है मानो कच्चा ही निगल जायेगा। आक्रमणकारी डरकर भाग जाता है तो भुनगा मौज से दूसरी तरफ चल देता है। इसे प्रकृति का प्रशिक्षण न कहा जाये तो और क्या कहा जाये?
कार्बोलिक एसिड एक जहरीला रसायन है इसे खाकर कोई जिन्दा नहीं रह सकता। उसकी मात्रा अपने स्वाभाविक विकास दर से बढ़ती रहती तो सारा संसार विषमय हो जाता। फिर बात क्या है जो अभी तक पृथ्वी अमृतत्व से ओत-प्रोत है। प्रोफेसर पी.जी. ग्रे नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसकी शोध की तो पाया कि मिट्टी में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं और इस तरह वे धरती माता को विषाक्त होने से बचा लेते हैं ऐसे कीटाणु एक दो नहीं 200 के लगभग तो अब तक खोजे भी जा चुके हैं। एक यह नन्हें कीटाणु हैं जो सामान्य होते हुए भी असामान्य कार्य करते हैं—भगवान् शिव के समान। एक है इन्सान जो संसार का विष—मानवता पर छाये विषैले वातावरण को मिटाने के लिए एक इन्च भी आगे नहीं बढ़ता भगवान् द्वारा प्रदत्त अपनी असामान्यता को कलंकित करता है। प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं का मनुष्य ने यदि सदुपयोग किया होता तो निस्सन्देह यह धरती तथाकथित स्वर्ग से कम नहीं वरन् अधिक ही साधन-सुविधाओं और सुख-शान्ति की प्रचुरताओं से भरी पूरी दीखती। इच्छा मात्र से अभीष्ट उपलब्धि
प्राणियों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं उनकी शारीरिक, मानसिक शक्तियों तथा भौतिक परिस्थितियों का सृजन करती हैं इस तथ्य को थोड़ा अधिक गहराई से विचार करने पर सहज ही जाना जा सकता है और उसके अनेकों प्रमाण पाये जा सकते हैं।
समझा जाता था कि वर्षा होने से वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, पर पाया यह गया है कि वृक्षों की आवश्यकता उधर उड़ने वाले बादलों को पकड़ कर घसीट लाती हैं और उसे अपने क्षेत्र पर बरसाने के लिए उन्हें बाध्य करती हैं। कुछ दिन पूर्व जहां बड़े रेगिस्तान थे पानी नहीं बरसता था और बादल उधर से सूखे ही उड़ जाते थे, पर अब जब वहां वन लगा दिये गये हैं तो प्रकृति का पुराना क्रम बदल गया और अनायास ही वर्षा होने लगी है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में अब यह नया सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि वहां की वन सम्पदा बादलों पर बरसने के लिए दबाव डालती है। बादलों की तुलना में चेतना का अंश वृक्षों से अधिक है इसलिए वे विस्तार में बादलों से कम होते हुए भी सामर्थ्य में अधिक हैं। अतएव दोनों की खींचतान में चेतना का प्रतिनिधि वृक्ष ही भारी पड़ता है।
आत्म-रक्षा प्राणियों की एक महती आवश्यकता है। जीवों में जागरुकता और पराक्रम वृत्ति को जीवन्त बनाये रखने के लिए प्रकृति ने शत्रु पक्ष का निर्माण किया है। यदि सभी जीवों को शान्तिपूर्वक और सुरक्षित रहने की सुविधा न मिली होती तो फिर वे आलसी और प्रमादी होते चले जाते। उनमें जो स्फूर्ति और कुशलता पाई जाती है वे या तो विकसित ही न होती या फिर जल्दी ही समाप्त हो जातीं।
सिंह, व्याघ्र, सुअर, हाथी, मगर आदि विशालकाय जन्तु अपने पैने दांतों से आत्म-रक्षा करते हैं और उनकी सहायता से आहार भी प्राप्त करते हैं। सांप, बिच्छू, बर्रे, ततैया, मधुमक्खी आदि अपने डंक चुभो कर शत्रु को परास्त करते हैं। घोंघा, केंचुआ आदि के शरीर से जो दुर्गन्ध निकलती है उससे शत्रुओं की नाक बंद करके भागना पड़ता है। गेंडा, कछुआ, सीपी, घोंघा, शंख, आर्मेडिलो आदि की त्वचा पर जो कठोर कवच चढ़ा रहता है उससे उनकी बचत होती है। टिड्डे का घास का रंग, तितली फूलों का रंग, चीते पेड़-पत्तों की छाया जैसा चितकबरापन गिरगिट मौसमी परिवर्तन के अनुरूप अपना रंग बदलता है। ध्रुवीय भालू बर्फ जैसा श्वेत रंग अपनाकर समीपवर्ती वातावरण में अपने को आसानी से छिपा लेते हैं और शत्रु की पकड़ में नहीं आते। कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, कूड़ा-करकट आदि के रंग में अपने को रंग कर कितने ही प्राणी आत्म-रक्षा करते हैं। शार्क मछली बिजली के करेन्ट जैसा झटका मारने के लिए प्रसिद्ध है। कई प्राणियों की बनावट एवं मुद्रा ही ऐसी भयंकर होती है कि उसे देखकर शत्रु को बहुत समझ-बूझकर ही हमला करना पड़ता है।
शिकारी जानवरों को अधिक पराक्रम करना पड़ता है इस दृष्टि से उन्हें दांत, नाखून, पंजे ही असाधारण रूप से मजबूत नहीं मिले वरन् पूंछ तक की अपनी विशेषता है। यह अनुदान उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर प्रकृति से प्राप्त किये हैं।
शेर का वजन अधिक से अधिक 400 पौंड होता है जबकि गाय का वजन उससे दूना होता है। फिर भी शेर पूंछ के सन्तुलन से उसे मुंह में दबाये हुए 12 फुट ऊंची बाड़ को मजे में फांद जाता है।
प्राणियों की शरीर रचना और बुद्धि संस्थान भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता है संकल्प शक्ति, इच्छा तथा आवश्यकता। यह सम्वेदनाएं जिस प्राणी की जितनी तीव्र हैं वे उतने ही बड़े अनुदान प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को जो विभूतियां उपलब्ध हैं उनका कारण उसकी बढ़ी हुई संकल्प शक्ति ही मानी गई है।
प्रकृति परायण वृक्ष
प्रकृति ने कुछ कायदे कानून ऐसे बनाये हैं जो सृष्टि सन्तुलन की दृष्टि से नितान्त आवश्यक हैं। इन नियमों को न केवल मनुष्यों के लिए वरन् अन्य प्राणियों के लिए भी बनाया गया है। यहां तक कि वनस्पतियों के लिए भी।
मनुष्यों में बुद्धि धन, बल, प्रतिभा, भावना आदि की सम्पदाएं ऐसी हैं जिन्हें उसके व्यक्तित्व का बीज कहा जा सकता है। इसी के आधार पर हम ऊंचे उठते और आगे बढ़ते हैं। बीज सड़ा-गला हो तो उससे वंश वृद्धि न हो सकेगी। गुण, कर्म, स्वभाव की विभूतियां यदि स्वस्थ और समर्थ न हों तो कोई व्यक्ति प्रगति के पथ पर दूर तक अग्रसर न हो सकेगा। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि हमारी विभिन्न शारीरिक और मानसिक हलचलें इन बीज तत्वों को विकसित, परिष्कृत और पुष्ट करने के लिए ही होती हैं। भौतिक और आत्मिक सम्पदाओं से अधिकाधिक मावा में सम्पन्न होने की अभिलाषा स्वाभाविक मानी जाती है—वह बनी ही रहती है—और उनके लिए जाने अनजाने प्रयास चलते ही रहते हैं।
वनस्पति-जगत में भी यही प्रक्रिया अपने ढंग से उसी तरह पलती रहती है जिस तरह मनुष्यों में चलती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्म-विस्तार है। हम बड़े, विकसित हों और सुदूर क्षेत्र तक फैलें इसके लिए भांति-भांति के प्रयत्न पुरुषार्थ किये जाते हैं यहां तक कि युद्ध भी। आध्यात्मिक क्षेत्र में यही विस्तार वार आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ाकर सबमें अपने को और अपने में सबको देखने वाला तत्व दर्शन हृदयंगम किया जाता है। बीज तत्व का विकास और सत्ता का विस्तार करने के लिये हम मनुष्यों के विभिन्न क्रिया-कलापों को संजोया जाना देखते हैं। यदि यह दो प्रवृत्तियां न होतीं तो कदाचित पेट और प्रजनन जैसी निकृष्ट स्तर के जीवों में पाई जाने वाली तुच्छ हलचलों के अतिरिक्त हम और कुछ महत्वपूर्ण सोचने या करने में समर्थ ही न हो पाते। ठीक यही बात वनस्पति-जगत पर भी लागू होती है।
पौधे बढ़ते और विकसित होते हैं। अन्ततः उनकी प्रौढ़ता फलवती होती है और उन पर फल लगते लदते हैं। यह फल मनुष्यों सहित अन्य प्राणियों के लिये आहार का काम देते हैं पर जहां तक वृक्ष के लिए इन फलों का अपना उपयोग है वह उनकी बीज सत्ता को अक्षुण्ण रखने, परिपुष्ट बनाने और सुविस्तृत करने के उद्देश्य में ही सन्निहित देखी जा सकती है। वृक्ष मात्र परोपकार के लिए ही नहीं फलते, उनके अपने जीवन की सार्थकता भी फलवान होने में ही हैं।
फलों में गूदा भरा होता है और गूदे के भीतर बीज रहते हैं। यह बीज एक जगह इकट्ठे नहीं रखे रहते वरन् दूर-दूर तक फासले पर रहते हैं। पूरे वृक्ष पर एक ही फल नहीं लगता वरन् उनकी बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था क्यों की इस पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि प्रगति के आधार जिस प्रकार मनुष्य के लिए बनाये गये हैं, वैसे ही वृक्षों के लिए भी विनिर्मित किये गये हैं।
गूदे का उद्देश्य है—बीज को पोषण देना, परिपुष्ट करना, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचना। माता के गर्भ में जिस प्रकार भ्रूण पकता, पलता है उसी प्रकार फल के उदर में गूदे के मध्य बैठा हुआ बीज धीरे-धीरे सबल और समर्थ बनता रहता है। मानव जीवन के अधिक तर क्रिया-कलाप भौतिक उपार्जन के लिये होते हैं। इससे सुविधा सामग्री तो मिलती ही है साथ ही वे विशेषतायें, विभूतियां भी परिपक्व होती हैं जिनके आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में सफलतायें पाई जा सकती हैं—जिन्हें विकसित व्यक्तित्व की परिपुष्ट सत्ता कहते हैं।
एक वृक्ष अनेक फल और प्रत्येक फल में अनेक बीज इसलिये उत्पन्न करता है कि उसकी सत्ता को अधिकाधिक विस्तार करने का अवसर मिले। उसे सीमित दायरे में संकीर्णता की परिधि में ही आबद्ध रहकर अविकसित कहलाने का कलंक न सहना पड़े। आत्मविस्तार बिना न तो आत्म-सन्तोष मिल सकता है और न आत्मगौरव। जब मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर—क्षुद्रता से महानता की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है तो वृक्ष भी उसी प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण क्यों न करें।
प्रत्येक बीज में एक पूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। परिपुष्ट होने के पश्चात् उसका अगला उद्देश्य वह रहता है कि उसी जाति के नये वृक्ष उत्पन्न करे। साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र की दृष्टि से समीपवर्ती सीमा बन्धन को लांघकर सुदूर क्षेत्रों तक अपनी सत्ता को सुविस्तृत बनाया जाय। फल के भीतर सारे बीज एक जगह ही इकट्ठे चिपके नहीं रहते। गूदे के भीतर वे थोड़ा-थोड़ा फासला देकर अलग-अलग जमे होते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि उन्हें पृथक्-पृथक् रूप से सुदूर क्षेत्र में जाने का और सुविस्तृत परिधि में विस्तार का अवसर मिले। यदि गूदे में सब बीज इकट्ठे रखे होते तो फल के पककर गिरने पर वे सभी एक जगह ही उगते। फलतः वे सभी एक दूसरे की खुराक छीनते—फैलने की जगह प्राप्त न कर पाते और ऐसे ही सूख मुरझाकर समाप्त हो आते। विस्तार के लिये यह आवश्यक है कि पुरखों के घर आंगन को छोड़कर अन्यत्र भी जाने और फैलने का प्रयत्न किया जाय।
वृक्ष की सत्ता फलों के माध्यम से यही सब करती रहती है। फलने और पकने के साथ-साथ उनकी वितरण चेष्टा भी उत्साहपूर्वक चलती है। गूदे में बीजों का स्थान अलग-अलग था भी इसीलिये कि उनके वितरण की व्यवस्था बन सके। आहार में प्रायः गूदा ही काम आता है। बीज कड़े होते हैं इसलिये वे फेंक दिये जाते हैं या संग्रह कर लिये जाते हैं। गूदा समाप्त हो जाने पर भी बीजों का अस्तित्व बना रहता है। यदि उन्हें पीसकर नहीं खाया गया है तो चबाने पर भी उनमें से अधिकांश साबुत बच जाते हैं। पेट में भी कम ही पचते हैं। मल मार्ग से निकल कर वे पृथ्वी पर बिखर जाते हैं और इधर-उधर छितराते धक्के खाते और वृद्धि करते हैं।
मनुष्य जीवन की प्रगति के भी दो आधार हैं एक भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हुए अपने में गुण, कर्म, स्वभावपरक बीज सत्ता को परिपुष्ट करना और दूसरा उस पुष्ट सत्ता को सुविस्तृत क्षेत्र में वितरण करके उन विभूतियों को दूर-दूर तक बिखेरना-विकसित करना। प्रथम चरण को शक्ति संचय कह सकते हैं और दूसरे चरण को सेवा साधना। बल-वृद्धि का, सामर्थ्य सम्पादन का उद्देश्य यही हो सकता है कि उनके वितरण विस्तार का लाभ सुदूर क्षेत्रों को मिले। जो लोग शरीर या परिवार के भीतर ही अपनी प्रतिभा का लाभ सीमित किये बैठे रहते हैं उन्हें गूदे के भीतर ही पहुंचाने वाले बीज की उपमा दी जाती है।
गूदे में पककर विकसित हुए बीज सुदूर क्षेत्रों तक फैले इसके लिये प्रकृति ने अनेकों प्रकार की व्यवस्थायें की हैं। प्राणियों द्वारा उनका खाया जाना और मल विसर्जन के साथ उनका दूर-दूर जा पहुंचना प्रत्यक्ष ही है। कई बीज फेंके या संग्रह करने पर किसी न किसी प्रकार वंश वृद्धि करने का अवसर पाने में सफल हो जाते हैं। बीजों का व्यवसाय भी होता है। अनाज की तरह अन्य बीज भी खरीदे-बेचे जाते हैं और वे यहां से वहां की यात्रा करते हैं। यह तो प्रचलित व्यवस्था हुई प्रकृति भी इस दिशा में भारी योगदान करती है और तरह-तरह के ऐसे साधन जुटाती है जिससे वह उत्पन्न हुई बीज सम्पदा किसी एक स्थान तक सीमित होकर न रह जाय वरन् उसे सुदूर क्षेत्रों में वितरित होने का अवसर मिले।
हवा असंख्यों बीजों को अपने साथ उड़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाती है। इस स्तर के हलके बीजों की वनस्पति जगत में कमी नहीं है। ‘कुनैन’ जिस सिनकोना पौधे से बनती है उस के बीज इतने हलके होते हैं कि एक औंस में 70 हजार तोले जा सकें। आर्किडो के बीज इससे भी हलके होते हैं। इनकी बनावट भी ऐसी होती है जैसे पक्षी के परों की। हलकापन और बनावट की विशेषता दोनों के कारण हवा उन्हें आसानी से उड़ा ले जाती है और कहीं से कहीं ले जाकर पटकती है। कुछ बड़े और भारी बीजों में सूर्यमुखी, डोंडिलिओन, सौक्स, बेलकुन, आक, सेंगर, सरकंडा आदि के बीज ऐसे हैं जो पैराशूट की तरह बने होते हैं वे हवा का तनिक-सा सहारा पाकर लम्बी उड़ान उड़ते हैं। नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। आक के बीज में जो रूई चिपकी होती है उससे उनका उड़ना कितना सुहावना लगता है। ब्लड फ्लावर, करची, न्यूमोनशिया, चाटियम जैसे पौधों के बीज भी रोएंदार होते हैं, जिनके कारण उनकी वायु यात्रा बड़ी सरल बन जाती है। अरलू, पराल, जरुल, सहजन, चीड़ के बीजों की बनावट भी पक्षियों के परों जैसी होती है। वे इच्छा से नहीं उड़ पाते पर हवा उनकी उड़ने की सारी व्यवस्था स्वयं जुटा देती है। कुछ तो पूरे फल ही उड़नशील होते हैं वे अपने बीज परिवार को लेकर क्षेत्र विस्तार का प्रयोजन पूरा करने के लिए हवा की सहायता से यात्रा करने पर उतर पड़ते हैं। ऐसे उड़ाक फलों में होलोक, मधुलता, जिमीकन्द, फ्रेक्सीनस, होपियामेपल, डिपटीरोकारपस, साल आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन में एलेथस की बनावट हवाई जहाज से बिलकुल मिलती-जुलती है, उसे देखकर यह असमंजस पड़ता है कि इन्हें देखकर हवाईजहाज बने या हवाईजहाज देखकर प्रकृति ने इन्हें बनाया है आंधियां-धूल, तिनके ही नहीं हल्के बीजों को भी अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और कहीं से कहीं उन्हें जा पटकती हैं, जड़ी-बूटियां प्रायः इसी प्रकार यहां से वहां जा पहुंचती हैं।
कुछ फल भी स्वार्थी मनुष्यों की तरह बड़े कृपण होते हैं। वे पके हुए बीजों को भी अपने सूखे खोखले में समेटे बैठे रहते हैं। स्वयं भले ही उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न हो पर दूसरों को लाभ न मिलने पाये, ऐसी मनोवृत्ति वाले मनुष्य ही नहीं फल भी दुनियां में मौजूद हैं। लाल पोस्त, सत्यानाशी, कुत्ताफूल, हंसलता तथा धतूरा इसी प्रकार के फल हैं। हवा जब इन्हें झकझोरती है तो खुद भी उलटने-पुलटने लगते हैं और बीजों को छोड़ने के लिये भी विवश होते हैं। स्वेच्छा से न सही बलात्कार से सही चलना उन्हें भी प्रकृति के कानूनों पर ही पड़ता है। संग्रही कोई बनना भी चाहे तो प्रकृति उसे वैसा करने की आज्ञा नहीं दे सकती। जो दिया गया है वह देने के लिये है जो यह नहीं जानते उन्हें इन फलों की तरह दुर्गति और बल प्रयोग का सामना करना पड़ता है।
पानी में उगने वाली वनस्पतियों के बीजों को लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। यह बीज हलके और हवा भरे स्पंज की तरह होते हैं, जिससे वे लहरों पर आसानी से तैरते रह सकें। नदियों और समुद्रों के तटों पर उगे हुए पेड़-पौधे भी अपने बीज, जल को समर्पित करके उन्हें अन्यत्र चले जाने की खुशी-खुशी छूट देते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो स्वजनों को अन्यत्र उपयोगी स्थानों पर जाने से रोककर घर की चहार-दीवारी में ही बन्द रखने के लिये मोहग्रस्त बना रहता है। कमल गट्ठे अक्सर पानी में तैरते हुए ही कहीं से कहीं जा सकते हैं। नारियल के फलों का पानी में गिरना और सहस्रों मील जन शून्य द्वीपों में जा उगना इसी प्रकार सम्भव हुआ है।
कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं। पक जाने और सूख जाने पर कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं। पक जाने और सूख जाने पर भी वे बीजों को बाहर नहीं निकलने देते। इस कठोर नियन्त्रण की उग्र प्रतिक्रिया होती है। बीज विद्रोह कर बैठते हैं और उस भीतरी तनाव से छिलका एक विस्फोट की तरह फटता है और बीज उछलकर बाहर निकल जाते हैं। गुलमेंहदी, बुलसेरिल, नाइटजेसमिल, अरण्ड, कालमेघ, वज्रदन्ती, फ्लाक्स, कंचनलता आदि फलों में अक्सर फटने और बीज उछलने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। प्रहलाद, विभीषण, कैकेयी, बालि आदि को अपने अभिभावकों एवं गुरुजनों के विरुद्ध इसी प्रकार विद्रोह करना पड़ा था। अनुचित प्रतिबन्ध के अहंकारी दुराग्रह अक्सर ऐसे ही विस्फोट उत्पन्न करते रहते हैं।
कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हवा, पानी, मनुष्य आदि की सहायता न पाने पर स्वयं ही अपनी प्रवृत्ति प्रेरणा से आत्म विस्तार का रास्ता अपने बलबूते बनाते हैं और जिसका भी अंचल हाथ लगे उसी को पकड़कर आगे चल पड़ते हैं। लटजीरा, गोखरू, वनऔखरा, चोर-कांटा, बुइया, ठोकरी, चित्रक आदि के फल अथवा बीज अपने कांटों के साथ पशु-पक्षियों के शरीरों एवं मनुष्यों के कपड़ों को पकड़ लेते हैं और उन पर सवारी गांठकर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं।
चींटियों, चूहे, गिलहरी आदि संग्रही प्रकृति के प्राणी बीजों को इकट्ठा करते हैं। बिलों में से छितरा कर वे फिर जहां-तहां जा पहुंचते हैं। पक्षियों के पैरों में चिपकी मिट्टी के साथ अथवा उनकी बीट के माध्यम से भी अनेक वनस्पतियां तथा वृक्ष लम्बी यात्रायें करते हुए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पहुंचते हैं।
वनस्पतियों और वृक्षों की यह आत्म-विस्तार की अपनी उपलब्धियों की सुदूर क्षेत्र में वितरण करने की प्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार पाई जाती है जैसी कि प्रकृति प्रेरणा मनुष्य को उपलब्ध है जो जीवन विद्या का मर्म जानते हैं वे अपनी आन्तरिक विशेषताओं को बीज सत्ता की तरह परिपक्व करने के लिए अपनी हलचलों का गूदा संजोये, साथ यह भी ध्यान रखें कि समस्त उपार्जन वितरण के लिए है ताकि संसार की शोभा-सुषमा का विस्तार होता रहे उसमें कमी न आने पाये।
इस प्रकृति प्रेरणा को ही ईश्वरीय विधान, उसकी विधि व्यवस्था धर्म या अध्यात्म कहा जा सकता है जो जिस सीमा तक इन प्रेरणाओं को हृदयंगम करने में सफल होते हैं उन्हें स्वयं सम्पन्न होती रहने वाली त्याग प्रक्रिया के अनुसार उसका लाभ सत्परिणाम के रूप में प्राप्त होता रहता है। इसी आधार पर कर्मफल की दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है। अच्छे कार्यों का, परमार्थिक प्रयासों का परिणाम सुखद आनन्ददायक होता है तो बुरे कार्यों, संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित प्रयासों का परिणाम भी दुखद व क्लेशदायी ही होता है, व्यक्तिवाद की संकीर्ण स्वार्थपरता को निरस्त करके लोकहित की जन कल्याण की सत्प्रवृत्तियों में अपनी विभूतियों को समर्पित करने की जीवन पद्धति का नाम ही मानवी संस्कृति है। इसके साथ यह भी समझने और विचार करने योग्य है कि परमात्मा की यह कारुणिक विधि-व्यवस्था सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगलमय है। उससे लाभ उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिये।