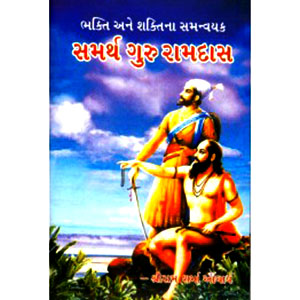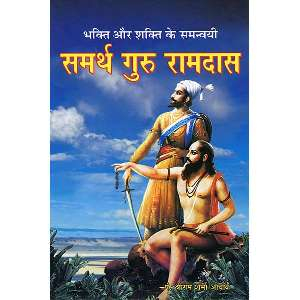समर्थ गुरु रामदास 
समर्थ गुरु रामदास
पर बहुत समय से भारतीय जनता धर्म के मूलस्वरूप को भूलकर उसे सामान्य-जीवन से कोई भिन्न बात मानने लग गई थी, जिससे लोग पूजा-पाठ जप-तप करते हुए भी सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहार में विपरीत आचरण करने लग गए थे। उदाहरण के लिए जिन लोगों ने अपने किसी स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाकर अथवा उनके साथ सहयोग करके देश को पराधीन कराया, जनता पर अत्याचार कराए, संपत्ति को लुटवाया उनको किसी ने अधार्मिक नहीं कहा। कारण यह कि इन समाज-विरोधी कार्यों को करते हुए भी वे अच्छी तरह से पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्रा, दान-दक्षिणा आदि का जिनको लोग 'धर्म-कृत्य' के नाम से पुकारते है, पालन करते रहते थे।
समर्थ गुरु रामदास ने (सन १६०८ से १६८२) धार्मिक भावना की इस त्रुटि को अनुभव किया और प्रवचनों तथा वाणियों में यह प्रतिपादित किया कि केवल धर्म और अध्यात्म की चर्चा करने का कोई महत्त्व नहीं। मनुस्मृति के अनुसार 'विद्वद्भि: सेवित: सद्भि' अर्थात् "जो कृत्य ज्ञानियों द्वारा सेवित या आचरित होते हैं, वे ही धर्म होते हैं।'' केवल चर्चा करने से कोई बात धर्म नहीं हो जाती, इसलिए उन्होंने जनता में धर्म के जिन सिद्धांतों का प्रचार किया तथा तदनुसार आचरण और लोक व्यवहार करने पर भी जोर दिया।
Write Your Comments Here:
- समर्थ गुरु रामदास
- विदेशी शासन से हिंदू धर्म में विकृति
- विवाह से विरक्ति और गृह-योग
- पंचवटी में साधन
- देश भ्रमण और सामाजिक स्थिति का निरीक्षण
- विभिन्न तीर्थों की यात्रा
- माता से भेंट
- समाज की रक्षा प्रथम कर्तव्य है
- आदर्श साधु जनसेवक के लक्षण
- राजनीतिक शिक्षा की आवश्यकता
- सामाजिक कर्तव्यों का पालन
- त्याग वृत्ति और सेवा भावना
- राजा भगवान् का नौकर होता है
- श्री समर्थ गुरु की क्षमा वृत्ति
- दान लेने में अरुचि
- अध्यात्मवाद का समर्थन