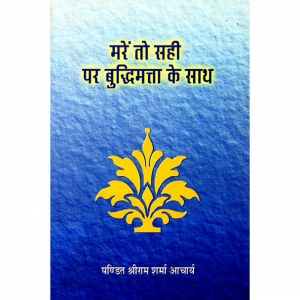मरे तो सही, पर बुद्धिमत्ता के साथ 
पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को क्रिया से जोड़ें
Read Scan Version
यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा-आस्था के अनुसार ही बनता-ढलता रहता है और उसी विनिर्मित व्यक्तित्व का प्रतिफल न केवल इहलोक में अपितु मरणोत्तर अवधि में परलोक में भी प्राप्त करता है। साथ ही जिस प्रकार इस लोक में दूसरों का सहयोग-सम्बल श्रद्धा-विश्वास व्यक्ति की प्रति एवं उत्कर्ष का आधार बनता है, उसी प्रकार परलोक में भी परिजनों का भावात्मक अनुदान जीवात्मा को शक्ति प्रदान करता है।
योग वशिष्ठ में बताया गया है कि मृत्यु के उपरान्त प्रेत यानी मरे हुए जीव अपने बन्धु-बांधवों के पिण्डदान द्वारा ही अपना शरीर बना हुआ अनुभव करते हैं— ‘‘आदी मृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात् । बंधु पिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ना इव वेदिनः ।।’’
(योगवशिष्ठ 3।52।27)
अर्थात् प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गये हैं और अब बन्धुओं के पिण्डदान से हमारा नया शरीर बना है।
स्पष्ट है कि यह अनुभूति भावात्मक की होती है। अतः पिण्डदान का वास्तविक महत्व उससे जुड़ी भावनाओं के ही कारण होता है। जिसके प्रति आत्मीयता होती है, उसके भावात्मक अनुदान से प्रेत प्रभावित होता है। क्योंकि मरणोत्तर जीवन की अनुभूतियां वासना और संस्कारों के प्रभाव की ही प्रतिच्छाया होती हैं। इसलिए जिससे आत्मीयता का संस्कार अंकित हो उसकी भावनायें परलोकस्थ जीव को प्रभावित करती है।
योगवशिष्ठ के अनुसार मरने के समय प्रत्येक जीव मूर्च्छा का अनुभव करता है। वह मूर्च्छा महाप्रलय की रात्रि के समान होती हैं। उसके उपरान्त प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने स्वप्न और संकल्प के अनुसार अपने परलोक की सृष्टि करता है यही बात श्लोकों में कही गई है—
‘‘मरणादिमयी मूर्च्छा प्रत्येके नानुभूयते । यैका तां विद्धि समते महाप्रलययामिनीम ।। तदन्ते तनुते सर्ग सर्व एव पृथक्-पृथक् । सहज स्वप्नसंकल्पान्संभ्रमाचल नृत्यवत् ।। (योगवशिष्ठ 3।40।31 व 32)
इसी संदर्भ में आगे बताया गया है— ‘‘स्ववासनानुसारेण प्रेता एतांव्यवस्थितम् । मूर्च्छान्तेऽनुभवन्त्यन्तः क्रमेणैवाक्रमेण च ।।
अर्थात् प्रेत अपनी-अपनी वासना के अनुसार ही भावनात्मक उतार-चढ़ावों का अनुभव करते हैं। मरे हुए व्यक्ति की प्रेतावस्था में जिन लोगों से आसक्ति जुड़ी रहती है, उनकी भाव-संवेदनायें और उनकी परिस्थितियां मनःस्थितियां प्रेतों को तीव्रता से प्रभावित करती हैं। पिण्डदान और श्राद्ध कर्म का महत्व यही है कि उन क्रियाओं के साथ-साथ जो भावनायें जुड़ी होती हैं, वे प्रेतों-पितरों को स्पर्श करती हैं। इसी प्रकार पितरों के संस्कारों के अनुरूप अपने प्रियपात्रों की स्थितियां उन्हें आन्दोलित करती हैं। जिनका यमलोक, यमदूत आदि पर विश्वास है, उन्हें वे उसी रूप में दिखाई पड़ती हैं। जिनकी किसी अन्य प्रकार की आस्था है, उन्हें वैसी अनुभूति होती है—ईसा या जिब्राइल या देवदूत या प्रकाशपिण्ड या घोर अन्धकार आदि के परिदृश्य इसी आधार पर सम्मुख आते हैं।
जिन पितरों की पिण्डदान-प्रक्रिया में आस्था होती है, वे उसकी अपेक्षा भी करते हैं और उस अपेक्षा की पूर्ति न होने से उन्हें क्लेश का अनुभव भी होता है।
‘रघुवंश’ में कालिदास ने राजा दिलीप के पितरों की इसी अनुभूति को व्यक्त किया है। दिलीप के सन्तान नहीं थी। स्वयं राजा दिलीप तो पितरों को श्राद्ध पक्ष एवं श्राद्ध पर्वों पर नियमपूर्वक पिण्डदान देते थे। किन्तु उनके सन्तान थी नहीं। अतः दिलीप को मृत्यु के बाद अपने लिए पिण्डदान की परम्परा लुप्त हो जाने की आशंका उनके पितरों को होने लगी थी। इसी का वर्णन कालिदास ने किया है। उन्होंने रघुवंश में दिलीप को अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हुए बतलाया है—
नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः । न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रहतत्पराः ।। (रघुवंश 1।66)
अर्थात् ‘हे गुरुवर! मेरे बाद पिण्ड का लोप देखने वाले, स्वधा इकट्ठी करने में लगे हुए मेरे पूर्वज, श्राद्ध में इच्छापूर्वक भोजन के लिए उत्साह नहीं कर रहे हैं।’
अर्थात् ‘‘मुझे पुत्र रहित देखकर मेरे बाद उन्हें पिण्डदान प्राप्त होना सम्भव न होगा, ऐसी चिन्ता में डूबे पितर मेरे द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं रख पा रहे।’’
पुत्र-प्राप्ति के आकांक्षी दिलीप ने पितरों की अपेक्षा का वर्णन करते हुए आगे कहा—
मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया । पयः पूर्वैः स्वनिःश्वासैः कवोष्णामपभुज्यते ।। (1।57)
मैं जो श्राद्ध-तर्पण करता हूं, उस तर्पण जल से मेरे पितर आंतरिक शीतलता का समुचित अनुभव नहीं कर पाते। यह सोचकर कि मेरे बाद तो यह जल दुर्बल ही हो जायगा, वे जो दुःख भरे निःश्वास छोड़ते हैं उसकी दाहकता मानो उस तर्पण-सलिल को कुछ गरम कर देती है।
इस कथन से स्पष्ट होता है कि परलोक स्थित पितृगणों का अपने परिजनों से आत्मीयतापूर्ण लगाव होता है और उनसे वे अपेक्षाएं भी रखते हैं। अपेक्षाओं की पूर्ति से उन्हें प्रसन्नता तथा अपेक्षाएं अपूर्ण रहने या उनके विपरीत आचरण होने पर निकलता, शोक संताप की अनुभूतियां होती हैं।
ऐसा नहीं है कि पितर चौबीसों घंटे घर-परिवार के आसपास ही मंडराते रहते हों तथा और कोई भी काम नहीं करते हों। वे अपने संस्कारों और आकांक्षाओं के अनुरूप भाव-लोक में रहते और विविध प्रकार की अनुभूतियां करते हैं। साथ ही अपने आसक्ति के ही कारण वे पूर्व के घर-परिवार की भी परिक्रमा कर जाते हैं। इस आने-जाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। क्योंकि यह सारी यात्रा संकल्पात्मक मन ही करता है। अतः परिजनों के भावों तथा स्थितियों के प्रवाह से वे परिचित रहते हैं। इसी प्रकार वे भावनाएं-संवेदनाएं जो पूर्वजों को लक्ष्य रखकर उत्पन्न होती तथा अभिव्यक्त होती हैं सूक्ष्म कंपनों के रूप में वातावरण में फैल जाती हैं तथा उन पितरों पूर्वजों तक पहुंच जाती हैं जिनका लगाव अभी भी अपने मृत्यु पूर्व के कुटुम्बियों से होता है। जिन पूर्वजों की संसक्ति उन पहले के रिश्तों के प्रति समाप्त हो चुकी होती है, उन तक न तो इन भाव-संवेदनाओं का ही कोई प्रभाव पहुंचता है, न ही उन्हें उन लोगों की, जो कभी उनके परिजन थे चिंता ही रहती। पर ऐसे मुक्त स्वभाव लोग थोड़े ही होते हैं और पूर्वकृत क्रियाओं-इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त आत्माएं नया जन्म भी ग्रहण कर चुकी होती हैं। अतः पितर नहीं रह जातीं। वे तो किसी के घर में आंगन में किलकारी भर रही होती हैं या वयस्क होकर अपने दायित्व निभा रही होती हैं। उनकी बात ही भिन्न है। किंतु परिजनों के प्रति ममत्व-शेष पितरों को अपेक्षाएं भी रहती हैं और रुचि भी रहती है। रुचि रखने के कारण वे अदृश्य सहायकों के रूप में काम करते हैं। ऐसों की अपेक्षाओं की पूर्ति प्रत्येक का कर्त्तव्य है। यह अपेक्षा-पूर्ति करना ही श्राद्ध-कर्म है।
श्राद्ध और तर्पण
भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म में श्राद्ध का अपना विशेष स्थान है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है और उसी से उसके गुप्त तात्पर्य पर प्रकाश पड़ता है। सत्कर्मों के लिए, सत्पुरुषों के लिए आदर की, कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। जिस व्यक्ति ने हमारे साथ उपकार किया है, हम उसका श्रद्धा सहित स्मरण करते हैं। इस स्मरण में भजन-पूजन के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था भी रहती है। यह सम्मिलित रूप श्रद्धा कहलाता है। श्राद्ध एक प्रकार से मृत पूज्य व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की भावना स्पष्ट करना है गुरुजनों के चरण स्पर्श, अभिनन्दन, सेवा आदि भावों की वृद्धि हमारे यहां महत्वपूर्ण मानी गई है। जब तक गुरुजन रहें, उनके प्रति कृतज्ञता चलती रहती है, स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् भी यही श्रद्धा कायम रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात् पितृ पक्षों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन, पर्व समारोहों पर श्राद्ध करने का श्रुति-स्मृतियों में विधान पाया जाता है। नित्य की संध्या के साथ तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भर कर कृतज्ञता के भाव से भर कर हम स्वर्गीय पितृ-देवों के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता, अभिनन्दन सभी का मिश्रित रूप हमारे श्राद्ध हैं।
श्राद्धों के द्वारा हमारी संस्कृति ने श्रद्धा तत्व को जीवित रखने का प्रयत्न किया है। जीवित पितृओं को तो हम सेवा-पूजा आराधना से प्रसन्न कर लेते हैं, पर स्वर्गीय पितरों का कृतज्ञता प्रकट करने का यही उपाय है। हिन्दू श्राद्ध करके ही मृतकों के उपकार, प्रेम, आत्मीयता से कृतज्ञ हो जाता है।
हिन्दू संस्कृति की उदारता महान् हैं। उसमें संकीर्णता कहीं नहीं है। कर्मकाण्डों में आधे से अधिक श्राद्धतत्व भरा पड़ा है। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुंआ, तालाब, नदी, मरघट, खेत, खलिहान, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों तक के प्रति हम अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। विवाह संस्कारों के अवसरों पर नाली या घूरे तक की पूजा होती है। वृक्षों में तुलसी, पीपल, बाड़, आंवला आदि तथा पशुओं में गौ, बैल, घोड़ा, हाथी तक पूजे जाते हैं।
श्राद्ध किस तत्व पर टिका है? शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीव का आस्तित्व नहीं मिटता। वह सूक्ष्म रूप में हमारे चारों ओर वातावरण में घूमते रहते हैं। जीव का फिर भी अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ ममत्व रह जाता है। सूक्ष्म आत्माएं आसानी से सब लोकों से आकर हमारे चारों ओर चक्कर लगाया करती हैं। हमारे विचार और भावनाएं इस सूक्ष्म वातावरण में फैलते हैं। इन्हें हम जिस तेजी से बाहर के वातावरण में फेंकते हैं, ये उसी गति से दूर-दूर तक फैल जाते हैं। अतः श्राद्ध में प्रकट किये गये पूर्वजों के प्रति हमारे आत्मीयता, सद्भावना, कृतज्ञता के भाव उन आत्माओं के पास पहुंच जाते हैं। उसे इनसे सुख, शान्ति, प्रसन्नता और स्वस्थता मिलती है।
इसी प्रकार तर्पण का वह जल पितरों के चरणों में एक प्रकार की श्रद्धांजलि माना गया है। यद्यपि यह जल तो यहीं गिर जाता है, पर जल ग्रहण करते समय हमारे मन में जो पवित्र कृतज्ञता के भाव आते हैं, उनका बड़ा महत्व है। हमारे मन की संकीर्णता, दुष्टता, ईर्ष्या, द्वेष आदि दूषित तमोगुणी नीच भावनाएं नष्ट होती हैं और प्रेम, त्याग, कृतज्ञता के भाव फैलते हैं। मन में पितरों की उपकारमयी, स्नेहमयी देवोपम मूर्तियां आती हैं। सद्विचार को अनुकूल बनाना ही पुरुषार्थ है। अभ्यास से विचार अनुकूल या प्रतिकूल बनते हैं। जो पुरुष जिस प्रकार के विचार बार-बार मन में लाता है, वह उसी प्रकार का स्वयं बनता है। श्राद्ध और तर्पण में कृतज्ञता, उपकार, प्रेम, त्याग आदि की सद्भावनाएं हमारे मन में आती हैं और हमें सुख-संतोष प्राप्त होता है। कृतज्ञता से इच्छा शक्ति बलवान् बनती है। श्रद्धा की भावना बढ़ती जाती है। सात्विक, परमार्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हमारी उच्च वृत्तियां पनपती हैं। प्रतिवर्ष श्राद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जो उपकारी पूजनीय एवं आत्मीय पुरुष स्वर्ग सिधार गये हैं, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रहना और प्रकट करना चाहिए।
पुत्र शब्द का एक अर्थ यह भी बताया जाता है कि जो पुरखों का नरक से त्राण करे, वह पुत्र। गरुड़ पुराण में कहा गया है—
नरकात्पितरं त्रायेत् तेन पुत्र इति स्मृतः ।।’’ (प्रेतकल्प 24।10)
अर्थात् नरक से पितरों को उबारता है, इसलिए उसे पुत्र कहा गया है। आगे कहा गया है— ‘‘दह्य मानस्य प्रेतस्य स्वजनैर्यैर्जजाञ्जलिः । दीयते प्रीतरूपोऽसौ प्रेतो याति यमालयम् ।।’’ (प्रेतकल्प 24।12)
अर्थात् दाह किये गये पितरों के स्वजन उसे जो भावनापूर्ण जलांजलि देते हैं उससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती और प्रसन्न होकर उच्चस्थ लोकों को गमन करते हैं। धर्म की गति सूक्ष्म कही गई है। अतः श्राद्ध कर्म के संस्कारों का सूक्ष्म निहितार्थ समझना ही धर्म है। स्थूल अर्थ मात्र का ग्रहण भ्रांति है। मात्र स्थूल कर्मकाण्डों से आत्मा का परलोक में कल्याण होना असम्भव है। क्योंकि स्थूल वस्तुएं वहां तक पहुंच सकने का प्रश्न ही नहीं और फिर वस्तुओं से तो इस लोक में भी किसी की तृप्ति नहीं होती। अधिकाधिक अतृप्ति ही बढ़ती है। अतः पूर्वजों के नाम पर कुछ वस्तुएं किसी कर्मकांड के साथ अर्पित कर देने भर से उनके तृप्त होने की विचित्र कल्पना करने के स्थान पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भावना द्वारा ही उन्हें भावात्मक तृप्ति पहुंचाने का प्रयास उचित है।
छोड़े हुए उत्तरदायित्व पूरे करें
पितरों को तृप्त कर सकने में समर्थ वास्तविक श्राद्धकर्म वह है, जो उनके छोड़े हुए उत्तरदायित्व को पूरा करने वाला हो। श्राद्ध की सही पृष्ठभूमि यही है। मरने के उपरान्त प्रत्येक जीव एक विश्राम निद्रा में कुछ समय से लिए चला जाता है। यदि अन्तःकरण शान्त और सन्तुलित हुआ तो उस स्थिति में सुसंस्कारों की प्रतिक्रिया स्वर्गीय सुखानुभूति जैसी होती रहती है यदि जीवन कुमार्गगामी, चिन्तन तथा क्रिया-कलाप में बीता है तो उस अवधि में डरावने नारकीय दृश्य दीखते रहेंगे और वैसी ही कष्टकारक अनुभूति होती रहेगी। मृत्यु और नवीन जन्म के बीच में जो थोड़ा अवकाश मिलता है उसमें आत्मा को यही स्वप्न दिखाई देते रहते हैं। इन्हें ही परलोक गत स्वर्ग नरक कहा जा सकता है स्वर्गीय दृश्य देखकर सुखद सन्तुष्ट निद्रा पूरी करके जगा हुआ जीव ताजगी और स्फूर्ति लिए होता है और नवीन जन्म में प्रगतिशील मनःस्थिति तथा परिस्थिति प्राप्त करता है। इसके विपरीत नरक के दृश्यों से डरता, कांपता आधा अधूरा विश्राम लेकर नये शरीर में प्रवेश हुआ प्राणी मन्द बुद्धि, कुसंस्कारी एवं हीन व्यक्तित्व का होता है वैसे ही घटिया वातावरण में उसे जन्म भी मिलता है। स्वर्ग-नरक और पुनर्जन्म में कैसी अनुभूति मिलेगी, कैसी स्थिति रहेगी इसे जानने के लिए किसी व्यक्ति का जीवन-क्रम किस प्रकार व्यतीत हुआ है इसे देखना होगा।
उस अवधि के अनुभवों का मुख्य आधार तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के संचित कर्म-संस्कार ही होते हैं। किन्तु परिजनों का भी उसमें योगदान हो सकता है। स्वप्न संवेदन भी आकस्मिक और अकारण नहीं होते। उसी प्रकार विश्राम की इस अवधि की अनुभूतियां भी सकारण और क्रमबद्ध होती हैं। अपने सद्भावनाओं, सत्प्रयासों से पूर्वजों की अनुभूतियों को सुखद बनाना प्रत्येक परिजन का कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति ही श्राद्ध कर्म है।
पितरों का कल्याण चाहने वाली सन्तान को उनके प्रति श्रद्धा को सक्रिय आचरण से जोड़ना चाहिए। यही सच्चा श्राद्ध-संस्कार हैं। ताकि विश्राम की अवधि में पितर गहरी मीठी नींद और सुन्दर, शुभ सपने ले सकें और नई ताजगी, नई स्फूर्ति प्राप्त कर सकें।
मृत्यु जीवनावस्था का रूपांतर मात्र है। व्यक्ति-चेतना अक्षय-अविनाशी विराट ब्रह्म-चेतना का ही अंश है, अतः अविनाशी है। संस्कारों-वासनाओं तथा सृष्टि के अटल नियमों के अनुसार ही व्यक्ति की स्थिति, गति तथा परिणति होती रहती है। अतः जीवन और मृत्यु के सही स्वरूप को समझने तथा तदनुसार सदैव स्वधर्म-आचरण करने में ही मनुष्य-जीवन की सार्थकता है। मृत्यु के लिए शोक करने जैसी कहीं कोई भी बात नहीं है। वह तो एक अनिवार्य, सुनिश्चित और सुन्दर घटना-क्रम है। उसे भव्य सार्थक, गरिमामंडित और शांतिपूर्ण बनाने में ही बुद्धिमानी है, ताकि वह शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी और सन्तोष देने वाली विश्राम-अवधि सिद्ध हो तथा अगली यात्रा का आरम्भ उत्साह के साथ हो सके।
योग वशिष्ठ में बताया गया है कि मृत्यु के उपरान्त प्रेत यानी मरे हुए जीव अपने बन्धु-बांधवों के पिण्डदान द्वारा ही अपना शरीर बना हुआ अनुभव करते हैं— ‘‘आदी मृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात् । बंधु पिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ना इव वेदिनः ।।’’
(योगवशिष्ठ 3।52।27)
अर्थात् प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गये हैं और अब बन्धुओं के पिण्डदान से हमारा नया शरीर बना है।
स्पष्ट है कि यह अनुभूति भावात्मक की होती है। अतः पिण्डदान का वास्तविक महत्व उससे जुड़ी भावनाओं के ही कारण होता है। जिसके प्रति आत्मीयता होती है, उसके भावात्मक अनुदान से प्रेत प्रभावित होता है। क्योंकि मरणोत्तर जीवन की अनुभूतियां वासना और संस्कारों के प्रभाव की ही प्रतिच्छाया होती हैं। इसलिए जिससे आत्मीयता का संस्कार अंकित हो उसकी भावनायें परलोकस्थ जीव को प्रभावित करती है।
योगवशिष्ठ के अनुसार मरने के समय प्रत्येक जीव मूर्च्छा का अनुभव करता है। वह मूर्च्छा महाप्रलय की रात्रि के समान होती हैं। उसके उपरान्त प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने स्वप्न और संकल्प के अनुसार अपने परलोक की सृष्टि करता है यही बात श्लोकों में कही गई है—
‘‘मरणादिमयी मूर्च्छा प्रत्येके नानुभूयते । यैका तां विद्धि समते महाप्रलययामिनीम ।। तदन्ते तनुते सर्ग सर्व एव पृथक्-पृथक् । सहज स्वप्नसंकल्पान्संभ्रमाचल नृत्यवत् ।। (योगवशिष्ठ 3।40।31 व 32)
इसी संदर्भ में आगे बताया गया है— ‘‘स्ववासनानुसारेण प्रेता एतांव्यवस्थितम् । मूर्च्छान्तेऽनुभवन्त्यन्तः क्रमेणैवाक्रमेण च ।।
अर्थात् प्रेत अपनी-अपनी वासना के अनुसार ही भावनात्मक उतार-चढ़ावों का अनुभव करते हैं। मरे हुए व्यक्ति की प्रेतावस्था में जिन लोगों से आसक्ति जुड़ी रहती है, उनकी भाव-संवेदनायें और उनकी परिस्थितियां मनःस्थितियां प्रेतों को तीव्रता से प्रभावित करती हैं। पिण्डदान और श्राद्ध कर्म का महत्व यही है कि उन क्रियाओं के साथ-साथ जो भावनायें जुड़ी होती हैं, वे प्रेतों-पितरों को स्पर्श करती हैं। इसी प्रकार पितरों के संस्कारों के अनुरूप अपने प्रियपात्रों की स्थितियां उन्हें आन्दोलित करती हैं। जिनका यमलोक, यमदूत आदि पर विश्वास है, उन्हें वे उसी रूप में दिखाई पड़ती हैं। जिनकी किसी अन्य प्रकार की आस्था है, उन्हें वैसी अनुभूति होती है—ईसा या जिब्राइल या देवदूत या प्रकाशपिण्ड या घोर अन्धकार आदि के परिदृश्य इसी आधार पर सम्मुख आते हैं।
जिन पितरों की पिण्डदान-प्रक्रिया में आस्था होती है, वे उसकी अपेक्षा भी करते हैं और उस अपेक्षा की पूर्ति न होने से उन्हें क्लेश का अनुभव भी होता है।
‘रघुवंश’ में कालिदास ने राजा दिलीप के पितरों की इसी अनुभूति को व्यक्त किया है। दिलीप के सन्तान नहीं थी। स्वयं राजा दिलीप तो पितरों को श्राद्ध पक्ष एवं श्राद्ध पर्वों पर नियमपूर्वक पिण्डदान देते थे। किन्तु उनके सन्तान थी नहीं। अतः दिलीप को मृत्यु के बाद अपने लिए पिण्डदान की परम्परा लुप्त हो जाने की आशंका उनके पितरों को होने लगी थी। इसी का वर्णन कालिदास ने किया है। उन्होंने रघुवंश में दिलीप को अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हुए बतलाया है—
नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः । न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रहतत्पराः ।। (रघुवंश 1।66)
अर्थात् ‘हे गुरुवर! मेरे बाद पिण्ड का लोप देखने वाले, स्वधा इकट्ठी करने में लगे हुए मेरे पूर्वज, श्राद्ध में इच्छापूर्वक भोजन के लिए उत्साह नहीं कर रहे हैं।’
अर्थात् ‘‘मुझे पुत्र रहित देखकर मेरे बाद उन्हें पिण्डदान प्राप्त होना सम्भव न होगा, ऐसी चिन्ता में डूबे पितर मेरे द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं रख पा रहे।’’
पुत्र-प्राप्ति के आकांक्षी दिलीप ने पितरों की अपेक्षा का वर्णन करते हुए आगे कहा—
मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया । पयः पूर्वैः स्वनिःश्वासैः कवोष्णामपभुज्यते ।। (1।57)
मैं जो श्राद्ध-तर्पण करता हूं, उस तर्पण जल से मेरे पितर आंतरिक शीतलता का समुचित अनुभव नहीं कर पाते। यह सोचकर कि मेरे बाद तो यह जल दुर्बल ही हो जायगा, वे जो दुःख भरे निःश्वास छोड़ते हैं उसकी दाहकता मानो उस तर्पण-सलिल को कुछ गरम कर देती है।
इस कथन से स्पष्ट होता है कि परलोक स्थित पितृगणों का अपने परिजनों से आत्मीयतापूर्ण लगाव होता है और उनसे वे अपेक्षाएं भी रखते हैं। अपेक्षाओं की पूर्ति से उन्हें प्रसन्नता तथा अपेक्षाएं अपूर्ण रहने या उनके विपरीत आचरण होने पर निकलता, शोक संताप की अनुभूतियां होती हैं।
ऐसा नहीं है कि पितर चौबीसों घंटे घर-परिवार के आसपास ही मंडराते रहते हों तथा और कोई भी काम नहीं करते हों। वे अपने संस्कारों और आकांक्षाओं के अनुरूप भाव-लोक में रहते और विविध प्रकार की अनुभूतियां करते हैं। साथ ही अपने आसक्ति के ही कारण वे पूर्व के घर-परिवार की भी परिक्रमा कर जाते हैं। इस आने-जाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। क्योंकि यह सारी यात्रा संकल्पात्मक मन ही करता है। अतः परिजनों के भावों तथा स्थितियों के प्रवाह से वे परिचित रहते हैं। इसी प्रकार वे भावनाएं-संवेदनाएं जो पूर्वजों को लक्ष्य रखकर उत्पन्न होती तथा अभिव्यक्त होती हैं सूक्ष्म कंपनों के रूप में वातावरण में फैल जाती हैं तथा उन पितरों पूर्वजों तक पहुंच जाती हैं जिनका लगाव अभी भी अपने मृत्यु पूर्व के कुटुम्बियों से होता है। जिन पूर्वजों की संसक्ति उन पहले के रिश्तों के प्रति समाप्त हो चुकी होती है, उन तक न तो इन भाव-संवेदनाओं का ही कोई प्रभाव पहुंचता है, न ही उन्हें उन लोगों की, जो कभी उनके परिजन थे चिंता ही रहती। पर ऐसे मुक्त स्वभाव लोग थोड़े ही होते हैं और पूर्वकृत क्रियाओं-इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त आत्माएं नया जन्म भी ग्रहण कर चुकी होती हैं। अतः पितर नहीं रह जातीं। वे तो किसी के घर में आंगन में किलकारी भर रही होती हैं या वयस्क होकर अपने दायित्व निभा रही होती हैं। उनकी बात ही भिन्न है। किंतु परिजनों के प्रति ममत्व-शेष पितरों को अपेक्षाएं भी रहती हैं और रुचि भी रहती है। रुचि रखने के कारण वे अदृश्य सहायकों के रूप में काम करते हैं। ऐसों की अपेक्षाओं की पूर्ति प्रत्येक का कर्त्तव्य है। यह अपेक्षा-पूर्ति करना ही श्राद्ध-कर्म है।
श्राद्ध और तर्पण
भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म में श्राद्ध का अपना विशेष स्थान है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है और उसी से उसके गुप्त तात्पर्य पर प्रकाश पड़ता है। सत्कर्मों के लिए, सत्पुरुषों के लिए आदर की, कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। जिस व्यक्ति ने हमारे साथ उपकार किया है, हम उसका श्रद्धा सहित स्मरण करते हैं। इस स्मरण में भजन-पूजन के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था भी रहती है। यह सम्मिलित रूप श्रद्धा कहलाता है। श्राद्ध एक प्रकार से मृत पूज्य व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की भावना स्पष्ट करना है गुरुजनों के चरण स्पर्श, अभिनन्दन, सेवा आदि भावों की वृद्धि हमारे यहां महत्वपूर्ण मानी गई है। जब तक गुरुजन रहें, उनके प्रति कृतज्ञता चलती रहती है, स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् भी यही श्रद्धा कायम रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात् पितृ पक्षों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन, पर्व समारोहों पर श्राद्ध करने का श्रुति-स्मृतियों में विधान पाया जाता है। नित्य की संध्या के साथ तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भर कर कृतज्ञता के भाव से भर कर हम स्वर्गीय पितृ-देवों के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता, अभिनन्दन सभी का मिश्रित रूप हमारे श्राद्ध हैं।
श्राद्धों के द्वारा हमारी संस्कृति ने श्रद्धा तत्व को जीवित रखने का प्रयत्न किया है। जीवित पितृओं को तो हम सेवा-पूजा आराधना से प्रसन्न कर लेते हैं, पर स्वर्गीय पितरों का कृतज्ञता प्रकट करने का यही उपाय है। हिन्दू श्राद्ध करके ही मृतकों के उपकार, प्रेम, आत्मीयता से कृतज्ञ हो जाता है।
हिन्दू संस्कृति की उदारता महान् हैं। उसमें संकीर्णता कहीं नहीं है। कर्मकाण्डों में आधे से अधिक श्राद्धतत्व भरा पड़ा है। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुंआ, तालाब, नदी, मरघट, खेत, खलिहान, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों तक के प्रति हम अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। विवाह संस्कारों के अवसरों पर नाली या घूरे तक की पूजा होती है। वृक्षों में तुलसी, पीपल, बाड़, आंवला आदि तथा पशुओं में गौ, बैल, घोड़ा, हाथी तक पूजे जाते हैं।
श्राद्ध किस तत्व पर टिका है? शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीव का आस्तित्व नहीं मिटता। वह सूक्ष्म रूप में हमारे चारों ओर वातावरण में घूमते रहते हैं। जीव का फिर भी अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ ममत्व रह जाता है। सूक्ष्म आत्माएं आसानी से सब लोकों से आकर हमारे चारों ओर चक्कर लगाया करती हैं। हमारे विचार और भावनाएं इस सूक्ष्म वातावरण में फैलते हैं। इन्हें हम जिस तेजी से बाहर के वातावरण में फेंकते हैं, ये उसी गति से दूर-दूर तक फैल जाते हैं। अतः श्राद्ध में प्रकट किये गये पूर्वजों के प्रति हमारे आत्मीयता, सद्भावना, कृतज्ञता के भाव उन आत्माओं के पास पहुंच जाते हैं। उसे इनसे सुख, शान्ति, प्रसन्नता और स्वस्थता मिलती है।
इसी प्रकार तर्पण का वह जल पितरों के चरणों में एक प्रकार की श्रद्धांजलि माना गया है। यद्यपि यह जल तो यहीं गिर जाता है, पर जल ग्रहण करते समय हमारे मन में जो पवित्र कृतज्ञता के भाव आते हैं, उनका बड़ा महत्व है। हमारे मन की संकीर्णता, दुष्टता, ईर्ष्या, द्वेष आदि दूषित तमोगुणी नीच भावनाएं नष्ट होती हैं और प्रेम, त्याग, कृतज्ञता के भाव फैलते हैं। मन में पितरों की उपकारमयी, स्नेहमयी देवोपम मूर्तियां आती हैं। सद्विचार को अनुकूल बनाना ही पुरुषार्थ है। अभ्यास से विचार अनुकूल या प्रतिकूल बनते हैं। जो पुरुष जिस प्रकार के विचार बार-बार मन में लाता है, वह उसी प्रकार का स्वयं बनता है। श्राद्ध और तर्पण में कृतज्ञता, उपकार, प्रेम, त्याग आदि की सद्भावनाएं हमारे मन में आती हैं और हमें सुख-संतोष प्राप्त होता है। कृतज्ञता से इच्छा शक्ति बलवान् बनती है। श्रद्धा की भावना बढ़ती जाती है। सात्विक, परमार्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हमारी उच्च वृत्तियां पनपती हैं। प्रतिवर्ष श्राद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जो उपकारी पूजनीय एवं आत्मीय पुरुष स्वर्ग सिधार गये हैं, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रहना और प्रकट करना चाहिए।
पुत्र शब्द का एक अर्थ यह भी बताया जाता है कि जो पुरखों का नरक से त्राण करे, वह पुत्र। गरुड़ पुराण में कहा गया है—
नरकात्पितरं त्रायेत् तेन पुत्र इति स्मृतः ।।’’ (प्रेतकल्प 24।10)
अर्थात् नरक से पितरों को उबारता है, इसलिए उसे पुत्र कहा गया है। आगे कहा गया है— ‘‘दह्य मानस्य प्रेतस्य स्वजनैर्यैर्जजाञ्जलिः । दीयते प्रीतरूपोऽसौ प्रेतो याति यमालयम् ।।’’ (प्रेतकल्प 24।12)
अर्थात् दाह किये गये पितरों के स्वजन उसे जो भावनापूर्ण जलांजलि देते हैं उससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती और प्रसन्न होकर उच्चस्थ लोकों को गमन करते हैं। धर्म की गति सूक्ष्म कही गई है। अतः श्राद्ध कर्म के संस्कारों का सूक्ष्म निहितार्थ समझना ही धर्म है। स्थूल अर्थ मात्र का ग्रहण भ्रांति है। मात्र स्थूल कर्मकाण्डों से आत्मा का परलोक में कल्याण होना असम्भव है। क्योंकि स्थूल वस्तुएं वहां तक पहुंच सकने का प्रश्न ही नहीं और फिर वस्तुओं से तो इस लोक में भी किसी की तृप्ति नहीं होती। अधिकाधिक अतृप्ति ही बढ़ती है। अतः पूर्वजों के नाम पर कुछ वस्तुएं किसी कर्मकांड के साथ अर्पित कर देने भर से उनके तृप्त होने की विचित्र कल्पना करने के स्थान पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भावना द्वारा ही उन्हें भावात्मक तृप्ति पहुंचाने का प्रयास उचित है।
छोड़े हुए उत्तरदायित्व पूरे करें
पितरों को तृप्त कर सकने में समर्थ वास्तविक श्राद्धकर्म वह है, जो उनके छोड़े हुए उत्तरदायित्व को पूरा करने वाला हो। श्राद्ध की सही पृष्ठभूमि यही है। मरने के उपरान्त प्रत्येक जीव एक विश्राम निद्रा में कुछ समय से लिए चला जाता है। यदि अन्तःकरण शान्त और सन्तुलित हुआ तो उस स्थिति में सुसंस्कारों की प्रतिक्रिया स्वर्गीय सुखानुभूति जैसी होती रहती है यदि जीवन कुमार्गगामी, चिन्तन तथा क्रिया-कलाप में बीता है तो उस अवधि में डरावने नारकीय दृश्य दीखते रहेंगे और वैसी ही कष्टकारक अनुभूति होती रहेगी। मृत्यु और नवीन जन्म के बीच में जो थोड़ा अवकाश मिलता है उसमें आत्मा को यही स्वप्न दिखाई देते रहते हैं। इन्हें ही परलोक गत स्वर्ग नरक कहा जा सकता है स्वर्गीय दृश्य देखकर सुखद सन्तुष्ट निद्रा पूरी करके जगा हुआ जीव ताजगी और स्फूर्ति लिए होता है और नवीन जन्म में प्रगतिशील मनःस्थिति तथा परिस्थिति प्राप्त करता है। इसके विपरीत नरक के दृश्यों से डरता, कांपता आधा अधूरा विश्राम लेकर नये शरीर में प्रवेश हुआ प्राणी मन्द बुद्धि, कुसंस्कारी एवं हीन व्यक्तित्व का होता है वैसे ही घटिया वातावरण में उसे जन्म भी मिलता है। स्वर्ग-नरक और पुनर्जन्म में कैसी अनुभूति मिलेगी, कैसी स्थिति रहेगी इसे जानने के लिए किसी व्यक्ति का जीवन-क्रम किस प्रकार व्यतीत हुआ है इसे देखना होगा।
उस अवधि के अनुभवों का मुख्य आधार तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के संचित कर्म-संस्कार ही होते हैं। किन्तु परिजनों का भी उसमें योगदान हो सकता है। स्वप्न संवेदन भी आकस्मिक और अकारण नहीं होते। उसी प्रकार विश्राम की इस अवधि की अनुभूतियां भी सकारण और क्रमबद्ध होती हैं। अपने सद्भावनाओं, सत्प्रयासों से पूर्वजों की अनुभूतियों को सुखद बनाना प्रत्येक परिजन का कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति ही श्राद्ध कर्म है।
पितरों का कल्याण चाहने वाली सन्तान को उनके प्रति श्रद्धा को सक्रिय आचरण से जोड़ना चाहिए। यही सच्चा श्राद्ध-संस्कार हैं। ताकि विश्राम की अवधि में पितर गहरी मीठी नींद और सुन्दर, शुभ सपने ले सकें और नई ताजगी, नई स्फूर्ति प्राप्त कर सकें।
मृत्यु जीवनावस्था का रूपांतर मात्र है। व्यक्ति-चेतना अक्षय-अविनाशी विराट ब्रह्म-चेतना का ही अंश है, अतः अविनाशी है। संस्कारों-वासनाओं तथा सृष्टि के अटल नियमों के अनुसार ही व्यक्ति की स्थिति, गति तथा परिणति होती रहती है। अतः जीवन और मृत्यु के सही स्वरूप को समझने तथा तदनुसार सदैव स्वधर्म-आचरण करने में ही मनुष्य-जीवन की सार्थकता है। मृत्यु के लिए शोक करने जैसी कहीं कोई भी बात नहीं है। वह तो एक अनिवार्य, सुनिश्चित और सुन्दर घटना-क्रम है। उसे भव्य सार्थक, गरिमामंडित और शांतिपूर्ण बनाने में ही बुद्धिमानी है, ताकि वह शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी और सन्तोष देने वाली विश्राम-अवधि सिद्ध हो तथा अगली यात्रा का आरम्भ उत्साह के साथ हो सके।
Write Your Comments Here:
- धीरे-धीरे आती जाती मृत्यु समीप
- मृत्यु की मीठी गहरी नींद जरूरी
- अर्धमृत न रहें, पूर्ण जीवित बनें
- मरण सृजन का अभिनव पर्व—उल्लासप्रद उत्सव
- आसक्ति मनुष्य को मृत्यु के बाद भी घुमाती है
- मृतात्मा को क्षुब्ध नहीं, तृप्त करें
- सुदीर्घ विश्राम की अवधि को सार्थक बनाएं
- पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को क्रिया से जोड़ें