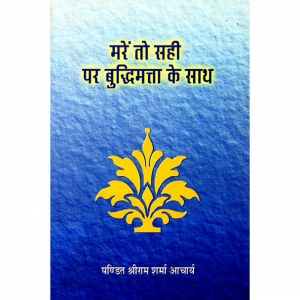मरे तो सही, पर बुद्धिमत्ता के साथ 
धीरे-धीरे आती जाती मृत्यु समीप
Read Scan Version
यों कहने को तो सभी कहते हैं कि जो जन्मा है सो मरेगा। इसलिये किसी की मृत्यु पर दुःख मनाते हुए भी यह नहीं कहा जाता है कि यह कोई अनहोनी घटना घट गई। देर सवेर में आगे-पीछे मरना तो सभी को है यह मान्यता रहने के कारण रोते-धोते अन्ततः सन्तोष कर ही लेते हैं। जब सभी को मरना है तो अपने स्वजन सम्बन्धी ही उस काल चक्र से कैसे बच सकते हैं?
लोक मान्यताओं की बात दूसरी है, पर विज्ञान के लिए यह प्रश्न काफी जटिल है। परमाणुओं की तरह जीवाणु भी अमरता के सन्निकट ही माने जाते हैं। जीवाणुओं की संरचना ऐसी है जो अपना प्रजनन और परिवर्तन क्रम चलाते हुये मूलसत्ता की अक्षुण्ण बनाये रहती है। जब मूल इकाई अमर है तो उसका समुदाय-शरीर क्यों मर जाता है? उलट-पुलटकर वह जीवित स्थिति में ही क्यों नहीं बना रहता? उनके बीच जब परस्पर सघनता बनाये रहने वाली चुम्बकीय क्षमता का अविरल स्रोत विद्यमान है तो कोशाओं के विसंगठित होने और बिखरने का क्या कारण है? थकान से गहरी नींद आने और नींद पूरी होने पर फिर जग पड़ने की तरह ही मरना और मरने के बाद फिर जी उठना क्यों सम्भव नहीं हो सकता?
बैक्टीरिया से लेकर अमीबा तक के दृश्यमान और अदृश्य जीवधारी अपने ही शरीर की उत्क्रान्ति करते हुए अपनी ही परिधि में जन्म-मरण का चक्र चलाते हुए प्रत्यक्षतः अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रहते हैं। फिर बड़े प्राणी ही क्यों मरते हैं? मनुष्य को ही क्यों मौत के मुंह में जाने के लिए विवश होना पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर में जर्मनी के जीव विज्ञानी आगस्ट वीजमान का कथन है कि जीव विकास की प्रगति श्रृंखला में प्राणियों का मरण तब से प्रारम्भ हुआ जब उनमें मेरुदण्ड और मस्तिष्क का विकास, विस्तार आरम्भ होने लगा। मेरुदण्ड भी वस्तुतः मस्तिष्क का ही एक पूंछ जैसा भाग है। मरण को कभी नाड़ी या हृदय की धड़कन के साथ जोड़ा जाता था, पर अब जीवन सत्ता में प्रधानता मस्तिष्क की ही मानी जाती है। हृदय समेत अन्य अवयव उसी के आज्ञानुवर्ती माने जाते हैं। अन्य अवयवों के निःचेष्ट हो जाने पर भी यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की हलचल विद्यमान है तो प्रत्यक्षतः उसे मृतक घोषित किये जाने पर भी उसमें जीवन का अस्तित्व माना जाता है और पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जाता है। मरने वालों में से बहुत से घोषित मृत्यु के दस मिनट पश्चात तक मस्तिष्कीय दृष्टि में जीवित पाये गये हैं और कृत्रिम धड़कन एवं श्वास-प्रश्वास की व्यवस्था करके प्राण लौटाने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। इनमें से कितनों को ही जीवित करने में सफलता भी मिल गई है।
मृत्यु भी प्रगतिक्रम की एक सीढ़ी कही जा सकती है। जड़ता में स्थायित्व है। परमाणु और तरंगों की सत्ता में ऊर्जा और हलचल तो है, पर मरण नहीं है। आरम्भिक स्तर के जीवधारियों में भी मरण संकट नहीं है। जीवाणुओं से लेकर एकेन्द्रिय जीवों तक अपनी सत्ता बनाये रहते हैं यों मरण का क्रम तो चलता रहता है, पर इससे उनके अस्तित्व के लिये चुनौती उत्पन्न नहीं होती। वे बिना टकराये और बिना किसी महत्वाकांक्षा के प्रकृति के प्रवाह क्रम में बहते रहते हैं। महत्वकांक्षाएं जहां प्रगति में सहायक हैं वहां उनमें यह खतरा भी मौजूद है कि प्रकृति ऐसे प्राणियों को अपनी सुव्यवस्था में बाधक समझें और उन्हें जल्दी ही अपना बिस्तर गोल करने के लिए रास्ता साफ करती है। मनुष्य के लिये मृत्यु संकट सम्भवतः इसीलिये अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक जटिल और कष्टकर बन गया है।
बीमारियों से मनुष्य का घिरा रहना भी उसका प्रकृति को चुनौती देने का ही दण्ड दुष्परिणाम है। उपभोग की मर्यादाओं का उल्लंघन शरीर संरचना के अनुरूप आचार संहिता न अपनाने से स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है और उसकी दुःखद प्रतिक्रिया आये दिन बीमार रहने के रूप में भुगतनी पड़ती है। जितना सरल, सौम्य, हलका और आवेश उत्तेजनाओं से रहित जीवन जिया जायगा उतना ही मृत्यु का भय और कष्ट हलका होता जायगा।
मौत भयानक या अवांछनीय ही हो, ऐसी बात नहीं। कई बार तो वह जीवन से भी अधिक मूल्यवान, सुखद और सत्परिणाम उत्पन्न करने वाली होती है। देश की सुरक्षा के लिये युद्ध क्षेत्र में जाने वालों में से कितनों को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है और वे उच्च आदर्शों के लिए इस प्रकार गंवाते हुये गर्व गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी इस वीरगति के लिये लोक श्रद्धा भी बरसती है। लोकहित के लिये प्रयत्नशील महानभावों में से कितनों को ही कठिनाइयों से जूझते हुये अकाल मृत्यु का ग्रास होना पड़ता है। कितने ईसा, सुकरात, गान्धी आदि की तरह प्रति पक्षियों द्वारा मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। गीता कहती है कि ऐसा मरण भाग्यवानों को ही उपलब्ध होता है। क्षत्रि धर्म में अनीति से संघर्ष करते हुये मिलने वाले मरण को यश और स्वर्ग देने वाला कहा गया है। मौत यदि बुरी ही होती तो उसे हर कोई कष्टकर ही अनुभव करता। तब गोली और फांसी के सामने दौड़ते हुये चले जाने के लिये कोई तैयार ही न होता वीर बलिदानियों की परम्परा ही समाप्त हो जाती।
कई बार तो जीवन और मौत के बीच कौन सुखद है यह चुनने में मनुष्य को मौत के पक्ष में अपना निर्णय देना पड़ता है। आत्महत्याएं उसी प्रकार के निर्णय का परिणाम होती हैं। समाज उसे किस दृष्टि से देखता है और कानून उसे कितना अवांछनीय दण्डनीय मानता है यह दूसरी बात है, पर जो इस प्रकार के भयानक निर्णय करते हैं और जिन्दगी से मौत को वरिष्ठ मान बैठते हैं उनके अपने भी तो कुछ तर्क होने ही चाहिये। भले ही उन्हें जन विवेक मान्यता न देता हो।
मनोविज्ञान शास्त्र को सुव्यवस्थित बनाने वाले डा. सिंग फ्रायड का नाम विश्व विख्यात है। उनकी समझदारी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हें जबड़े का कैन्सर हो गया था। यह लगातार 16 वर्ष तक चला। इतने समय में उस फोड़े का 33 बार आपरेशन हुआ। फिर भी वे उस असह्य पीड़ा से छुटकारा न पा सके। फलतः उन्होंने मार्फीन की सुई लगा ली और 83 वर्ष की आयु में स्वेच्छामरण को गौरवास्पद मानते हुये विदा हो गये।
इसी प्रकार एक असह्य पीड़ा से छटपटाते हुये असाध्य रोगी की दया भिक्षा स्वीकार करते हुये डा. विन्सेट मान्ट मेरिनो ने स्वेच्छामरण में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध करा दी थी, रोगी को पांच मिनट के भीतर ही चिरशान्ति का लाभ मिल गया। पर कानून ने इसे अपराध ही माना और चिकित्सक को न्यायालय का निर्धारित दण्ड भुगतना पड़ा। महात्मा गांधी ने भी साबरमती आश्रम में एक मृत्यु से छटपटाते हुये बछड़े को मरण की सुई लगाने की आज्ञा दें दी थी और उन्हें तीखे जनविरोध का सामना करना पड़ा था।
यहां स्वेच्छामरण के कानूनी और औचित्य पथ पर चर्चा नहीं हो रही है। देखा यह जा रहा है कि क्या कोई ऐसा भी समय आ सकता है जब जीवन से मरण को अधिक उपयुक्त माना जाय? मृत्यु दण्ड के अपराधियों के लिये भी न्याय परम्परा यही निर्धारण करती है कि उनके जीवित रहने की अपेक्षा मरण ही श्रेयस्कर है।
प्रसंग जीवन और मरण में से वरिष्ठता किसे दी जाय यह निर्णय करने का है। यहां सब कुछ सापेक्ष ही ठहरता है। उपयोगिता ही प्रधान है। न जीवन ही सदा सर्वदा उत्तम समझा जा सकता है और न मृत्यु को ही सर्वथा हेय ठहराया जा सकता है। दोनों ही अपने-अपने स्थान पर गुण-दोष की कसौटी पर कसे जाने के उपरान्त श्रेष्ठ समझे जा सकते हैं।
प्राणियों को इस मनःस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुये महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं—
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरम् । अन्ये स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम् ।।
अर्थात्—प्राणियों को निरन्तर मृत्यु मुख में जाते हुये आंखों से देखते हुये भी लोग अपनी स्थिरता का भ्रम पाल लेते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है?
इस विस्मरण के कारण मृत्यु का नाम सुनते ही साधारण व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। और एक क्षण के लिये वह जैसे मर सा जाता है। मृत्यु से डरने का मानव का स्वभाव सा बन गया है। साधारण सा रोग, मामूली सी घटना, शत्रु का विचार आदि शंका जनक संयोग आते ही कमजोर आदमी कांप उठता है और सोचने लगता है कि कहीं यह बीमारी हमारे प्राण न ले ले। कहीं वह शत्रु हमें मार डालने की न सोच रहा हो। सम्भव है वहां जाने से हम किसी घातक घटना के शिकार बन जायें मृत्यु के भय से मनुष्य खाने-पीने और प्रतिकूलताओं से जमकर मोर्चा लेने से डरता रहता है।
यही नहीं, किसी की मृत्यु देखकर, किसी दुर्घटना का समाचार सुनकर भी अपनी मृत्यु की शंका से आक्रांत हो जाता है। यहां तक कभी-कभी स्वयं भी अकेले में संसार की नश्वरता का विचार आते अथवा अपनी आयु के बीत गये वर्षों पर विचार करने से मृत्यु भय से उद्विग्न हो उठता है। अन्धेरे अथवा अपरिचित स्थानों में निर्भयता पूर्वक पदार्पण करने से भी उसे मृत्यु की शंका निरुत्साहित कर देती है। निःसन्देह मृत्यु का भय बड़ा ही व्यापक तथा चिरस्थायी होता है।
किन्तु, यदि इस मृत्यु भय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये तो यह बड़ा ही क्षुद्र तथा उपहासास्पद ही प्रतीत होगा। पहले तो जो अनिवार्य है अवश्यम्भावी है उसके विषम विषय में डरना क्या? जब मृत्यु अटल है और एक दिन सभी को मरना ही है तब उसके विषय में शंका का क्या प्रयोजन हो सकता है? यह बात किसी प्रकार भी समझ में न आने लायक नहीं है। हमारे पूर्वजों की एक लम्बी परम्परा मृत्यु के मुख में चली जा चुकी है और आगे भी आने वाली प्रजा उनका अनुसरण करती ही जायेगी तब बीच में हमें क्या अधिकार रह जाता है कि उस निश्चित नियति के प्रति भयाकुल अथवा शंकाकुल होते रहें। मृत्यु को यदि जीवन का अन्तिम एवं अपरिहार्य अतिथि मानकर उसकी ओर से निश्चिंत हो जायें तो न जाने अन्य कितने भयों से हम अनायास ही मुक्ति पा जाएं।
आवश्यकता मृत्यु से डरने की नहीं है और न ही उस अनिवार्य वास्तविकता की उपेक्षा करने की है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसलिये तो उसकी चिन्ता कर्म है जो निश्चित है, उसकी चिन्ता कैसी? उसके प्रति तो निश्चित ही रहना चाहिये। हां उसकी निश्चितता का स्मरण सदैव रखना चाहिये। मृत्यु से न तो डरें और न ही उसे भूलने की कोशिश करें। अपितु मृत्यु को जानें, समझें और स्मरण रखें। साथ ही जीवन को भी जानें तथा स्मरण रखें। अधिकांश लोग न तो जीवन की भव्यता का स्मरण रख पाते, न ही मृत्यु के गौरव को समझ पाते। मृत्यु अनायास आने वाली एक निश्चित घटना है और जीवन अनवरत बहने वाला एक अनन्त चेतना-प्रवाह है, ये दोनों ही तथ्य सदा स्मरण रखने योग्य हैं।
शरीर क्षय की आंतरिक क्रियाएं
शरीर-रचना जिन सूक्ष्म परमाणुओं से हुई है, उन्हें ‘जीव-कोश’ कहते हैं। जीव-कोशों से भरा हुआ कलल जीवन-रस (प्रोटोप्लाज्म) कहलाता है यह रस तेईस मौलिक तत्वों से बना है। इसी को जीवन का मूल आधार समझना चाहिये। मोटे तौर पर यह तत्व आहार से मिलते हैं। पर यह प्रतिपादन भी अपूर्ण है। क्योंकि जो तत्व आहार में होते ही नहीं, वे फिर जीवन-रस को कैसे प्राप्त होंगे? आश्चर्य यह है कि वे सभी तत्व जीवन-रस को उपलब्ध होते रहते हैं। भले ही आहार में उनका अभाव रहता हो।
जीव-कोश बढ़ते हैं और फिर एक से दो होते रहते हैं। जब तक यह वृद्धि एवं उत्पत्ति का क्रम चलता रहेगा, तब तक शरीर भी बढ़ता रहेगा। यह वृद्धि-उत्पत्ति रुकते ही शरीर की अभिवृद्धि भी रुक जाती है। इस प्रक्रिया में जब निर्बलता या गड़बड़ी उत्पन्न होती है, तो उसी क्रम से शरीर भी कमजोर या बीमार पड़ता है। अन्तरंग कोशीय जीवन पर ही बाह्य जीवन-मरण निर्भर है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, अवयवों की थकान, घिसट या विकृति भी बढ़ती है, इसका प्रभाव कोषों पर पड़ता है उनकी बाहरी शकल तो यथावत बनी रहती है पर भीतर का ‘जीवन रस’ घटता और सूखता जाता है, उसकी ताजगी और सशक्तता भी घट जाती है, यही बुढ़ापे का कारण है। जब जीवन रस अधिक घट जाता है या निकम्मा हो जाता है तो जीव कोश मरने लगते हैं यही मृत्यु का कारण है। देर में या जल्दी जब भी मौत होगी—किसी भी कारण से होगी शरीर के भीतर यही स्थिति पाई जायगी।
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर कानूनगो के नेतृत्व में इस प्रकार के अध्ययन के लिए एक टोली नियुक्त की थी कि बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार बताये जाने वाले एंजाइमों, हारमोनों, ऊतकों, कोशिकाओं, रासायनिक तत्वों एवं मनोभावों का इस संदर्भ में कितना हाथ है। अध्ययन से पता चला—
(1) देखा गया है कि आयु वृद्धि के साथ-साथ उपापचयन एवं न्यूरोह्यू मोरल नियमन प्रणाली में परिवर्तन होने लगता है और कोमलता का स्थान कठोरता लेने लगती है यहीं से बुढ़ापा प्रारम्भ होता है। बालक की कोमलता किशोर अवस्था में घट जाती है और वह अपेक्षाकृत कठोर दीखने लगता है यह बुढ़ापे का ही प्रारम्भिक रूप है। (2) आनुवांशकी सिद्धान्त के अनुसार पैन्टक जीन्स भी अल्पायु दीर्घायु जरायुक्त यौवन, और यौवन युक्त जरा के लिए जिम्मेदार हैं। माता से 23 और पिता से 23 इस प्रकार 46 गुणसूत्रों में जुड़े हुए असंख्य ‘जीन्स’ शरीर में विद्यमान रहते हैं। इनमें भी वे बीज विद्यमान रहते हैं जो जवानी को देर तक बनाये रहें अथवा नई उम्र में ही बुढ़ापा खड़ा कर दें।
(3) संयोजी ऊतक हमारे सारे शरीर में फैले हैं। उनकी संख्या हड्डियों के सिरों से जुड़ी हुई मांस पेशियों में सबसे अधिक होती है। यह जोड़ ही हड्डियों का नियन्त्रण करते हैं। इन संयोजी ऊतकों में तीन अघुलनशील प्रोटीनें पाई जाती हैं। (1) कोलाजेन (2) इलास्टिन (3) रेडिक्रलित। इनमें से कोलाजेन शरीर का एक तिहाई भाग बनाती है और कोशिकाओं के बीच जोड़ का काम करती है। यह उपयोगिता होते हुए भी जब उसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो अमिनो अम्ल उभरता है और शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। (4) हमारे शरीर में प्रतिदिन अगणित कोशिकायें जन्मती और मरती हैं। किन्तु मस्तिष्क की तांत्रिक कोशिकाओं के बारे में यह बात नहीं है। उनका पुनर्निर्माण नहीं होता। मस्तिष्क में कोशिकायें प्रति घन सेन्टी मी. एक करोड़ के अनुपात में पाई जाती हैं। वे प्रति घण्टे एक हजार की औसत से मरती रहती हैं। इस प्रकार यह पूंजी क्रमशः घटती रहती है। बहुधा जीवन-काल में ही 10 प्रतिशत मस्तिष्क घट जाता है। यह पूंजी समाप्त होते चलने से शरीर पर मनःचेतना का नियन्त्रण घटता चलता है और वह कभी बुढ़ापे का निमित्त बन जाती है।
(5) हृदय, शिरायें, पेशियां, ग्रन्थियां, तांत्रिकी मृच्छिकायें जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को समर्थ बनाये रखने वाले रासायनिक पदार्थ घट जाते हैं। आयुवृद्धि के साथ-साथ रड्रिनेलिन, थायरोक्शिन, कोर्टिसोन, डिसौक्सीकौटिंकोटरीन इन्सुलीन, सैक्स हारमोनों जैसे तत्वों की कमी होने से वे अंग शिथिल पड़ जाते हैं। मस्तिष्क के अधः चेतन भाग हाईपोथेलेमस—का नियन्त्रण ढीला हो जाता है और यह बिखराव बुढ़ापे के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्कीय विद्युत तरंगें—अल्फा वेव—तब मन्द हो जाती हैं और बाल सफेद होने लगते हैं।
(6) डी.एन.ए. अणु शरीर की प्रोटीनों का ढांचा बनाता है। वह आयुवृद्धि के साथ-साथ भटकना शुरू करता है फलस्वरूप प्रोटीन वायोसिथेसिस प्रणाली लड़खड़ाने लगती है और बुढ़ापा आ घेरता है।
सोचा यह जा रहा है कि उपरोक्त अवरोधों को देर तक शरीर तन्त्र में प्रविष्ट न होने से रोकने के लिए क्या उपाय अपनाये जायं। रहन-सहन की आहार-विहार की क्या पद्धति निर्धारित की जाय ताकि विकृतियों का क्रम न्यूनतम बना रहे और यौवन की स्थिरता देर तक बनी रहे।
जीन फिनोल ने अपनी पुस्तक ‘दि फिलोसोफी आफ लोंग लाइफ’ में लिखा है—‘मृत्यु की दिशा में आधी यात्रा हम स्वाभाविक रीति से करते हैं और आधी अस्वाभाविक रीति से। स्वाभाविक वह है जिसमें एक नियत क्रम से वृद्धावस्था आती है और परिपक्व आयु भोगकर शरीर असमय बुढ़ापा हमीं बुलाते हैं। मृत्यु की गोद में चला जाता है, अस्वाभाविक वह जिसमें मनुष्य छोटी-मोटी बीमारियों के समय—बढ़ती आयु का लेखा-जोखा रखते हुए—अपनी आयु के मरने वालों की लिस्ट बनाकर यह सोचता रहता है कि अब मृत्यु का समय नजदीक आ गया। यह मान्यता यों महत्वहीन मालूम पड़ती है, पर सच्चाई यह है कि वह अन्तर्मन में एक सुनिश्चित संकल्प बनकर बैठ जाती है और मृत्यु को जल्दी ही कहीं से पकड़ कर ले आती है। संकल्पों से परिस्थितियों का उत्पादन एक सुनिश्चित सत्य है अतएव समय से पूर्व अस्वाभाविक मृत्यु के मुख में चला जाना भी एक यथार्थता ही है।
वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार मनुष्य एक अग्नि पिण्ड की तरह—जलते हुए दीपक की तरह है। आग ऑक्सीजन खाती है और कार्बन डायऑक्साइड गैस उगलती है। बिलकुल यही क्रम मनुष्य का भी है। उसकी श्वास प्रश्वांस क्रिया इसी क्रिया को सम्पन्न करती है। हमारा शरीर—जीवन की एक दिव्य अग्नि की तरह ही ज्वलन्त है। इस भट्टी में यदि उपयुक्त ईंधन पड़ता रहे और उन कारणों से बचा जा सके जो उसे ठण्डी कर देते हैं तो फिर मरने में आमतौर से जो उतावली हो जाती है वह न हो और देर तक जीवित रह सकना संभव हो जाय।
देर तक जीवित रह सकने के महत्वपूर्ण आधार जिन्दगी के साथ जुड़े हुये हैं, यदि उन्हें ठीक तरह संभाले, संजोये रखा जा सके। उद्धत आचरण और उच्छृंखल विचारों से बचा जा सके तो न केवल देर तक वरन् सुख पूर्वक जीवित रहने का आनन्द बिना किसी अड़चन के लिया जा सकता है। मौत के समीप लाने वाले कारण यों समय-समय पर सामने आते रहते हैं, पर वे ऐसे नहीं हैं जिन्हें निरस्त न किया जा सके। हम भीतर से हारते हैं तो बाहर से भी पराजय ही आ घेरती है। भीतर से थकते हैं तो चारों ओर से निराशा और असफलता की घटनाएं घिरती चली आती हैं।
असमय मरण और कुछ नहीं हमारी निरन्तर की भूलों का ही दुष्परिणाम है। यदि सतर्कता बरती जाय तो हम शताब्दियों तक जी सकते हैं और अन्तिम सांस तक हंसते-खेलते उल्लासपूर्ण मनःस्थिति में रह सकते हैं। ध्यान यदि आन्तरिक संतुलन का रखा जा सके तो बाहरी क्रिया-कलाप में रहने वालों अवांछनीय भूलें सहज सहज ही घटती और मिटती चली जायेंगी।
बुढ़ापा आयु के आधार पर नहीं विचारों के आधार पर आता है। यदि ऐसा न होता तो तीस वर्ष में लोग बूढ़े और सत्तर वर्ष के जवान क्यों दिखाई पड़ते?
वैज्ञानिक जेक्त लूटो ने कितने ही प्राणियों का शारीरिक तापमान गिराकर उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है और पाया है कि इससे इनका जीवन काल आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। उनका कथन है कि यदि मनुष्य का स्वाभाविक तापमान 98.6 से घटाकर आधा अर्थात् 49.3 किया जा सकें तो आयु 20 गुनी बढ़ सकती है। 70 वर्ष जीने योग्य शरीर को 1400 वर्ष जिन्दा रखा जा सकता है।
मानवी जीवकोशों की सुदृढ़ता को परखते हुए कोलंबिया विश्वविद्यालय के डा. एच.एस. सिक्स ने कहा है यदि स्नायु उत्तेजना और रासायनिक विकृतियों से शरीर की रक्षा की जा सके तो मनुष्य की संरचना उसे 800 वर्ष तक जीवित रहने का अवसर दें सकती है।
कार्नेट विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान ने अपने परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला है कि शारीरिक श्रम की तुलना में नीरस मानसिक श्रम से कहीं अधिक थकान आती है। खाद्य-पदार्थों में पाई जाने वाली ऊष्मा जिसे ‘कैलोरी’ कहते हैं यदि कम मात्रा में मिले तो थकान आवेगी। यह मान्यता भी अभी पूर्णतया निरस्त नहीं हुई है। पिछली शताब्दी के यह निष्कर्ष अभी भी दुहराये जाते हैं कि भोजन में ऊष्मा की मात्रा समुचित हो तो थकान से बचा जा सकता है और बुढ़ापा वस्तुतः थकान ही है। यह माना जाता है कि 150 पौण्ड वजन का कोई व्यक्ति सोते समय 65 कैलोरी प्रति घण्टा खर्च करता है। लेटे रहने में 77, पढ़ने में 100, टाइप करने जैसे कामों में 145, चलने-फिरने में 200 और कड़ा परिश्रम करने में 300 कैलोरी प्रति घण्टा के हिसाब से खर्च होती है।
डा. वाल्डविन के अनुसार मनुष्य शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री रहता है, पर उसे अनुकूल 68 डिग्री तापमान का वातावरण ही पड़ता है। इससे अधिक ठण्डक या गर्मी होने पर उसकी कैलोरी शक्ति अधिक मात्रा में खर्च होने लगती है और थकान जल्दी चढ़ती है। डा. डीनाल्ड ए. लेयर्ड के अनुसार कोलाहल भरे वातावरण में रहने वाले मनुष्य को 20 प्रतिशत थकान उस शोरगुल के कारण ही चढ़ती रहती है।
मेयोक्लीनिक के डा. केन्द्रिल ने कहा है चिड़चिड़ापन मनुष्य की थकान का सर्वविदित चिन्ह है। लेहीक्लीनिक के डा. एलेक का मत भी यही है—वे कहते हैं चिड़चिड़ा मनुष्य दया का पात्र है क्योंकि वस्तुतः वह गहरी थकान का मरीज होता है। उस पर क्रोध करने या बदला लेने से तो इस मरीज का और भी अहित होगा। थकान बढ़ेगी और बुढ़ापे की रफ्तार तेज होगी।
जीव विज्ञानियों के अनुसार मृत्यु एक प्रकार की अत्यधिक गहरी थकान अथवा इतनी प्रगाढ़ निद्रा है जिसमें गिरने के बाद फिर जागृत हो सकना सम्भव नहीं हो पाता। यदि इस थकान को दूर करने जितने समय तक सुरक्षित विश्राम की व्यवस्था बन जाय और जागने की अवधि तक शरीर के जीवाणुओं को मरने, सड़ने या सूखने से बचाया जा सके तो मृत्यु के बाद फिर कुछ समय बाद जी उठना सम्भव हो सकता है।
चेतना मरती नहीं थक जाती है। बुढ़ापे के कारण नाड़ी संस्थान की लचक घट जाती है कोशिकाओं का नवीनीकरण क्रम शिथिल हो जाता है। शरीर यन्त्र उन्हीं कारणों से कठोर एवं शिथिल होता चला जाता है। जीवनी शक्ति का इसी क्रम से ह्रास होता है और धीरे-धीरे बढ़ती हुई जराजीर्ण अवस्था मृत्यु के समीप तक जा पहुंचती है। इस कठोरता एवं शिथिलता की गति जितनी मन्द होगी उतने ही अधिक समय तक जीवित एवं सक्रिय रहा जा सकेगा। थकान धीरे-धीरे पैदा हो दीर्घजीवन का प्रधान सूत्र यही है। प्रगाढ़ विश्राम की सुविधा बीच-बीच में इस प्रकार मिलती रहे कि पिछले दिनों की क्षति को पूरा किया जा सके तो फिर यह सम्भव हो जायगा कि बहुत लम्बे समय तक जीवन बना रहे। हर रात को सोने और हर सवेरे उठने का क्रम एक मध्यावधि मरण एवं पुनर्जीवन हो तो है उसी सामान्य क्रम को विशेष उपचार से दीर्घकालीन बनाया जा सके तो कोशिकाओं पर छाई हुई थकान से उत्पन्न जरठता का निवारण हो सकता है और बूढ़े का फिर से जवान बन सकना शक्य बन सकता है।
तीस वर्ष तक हमारा शरीर निरन्तर बढ़ता है। इसके बाद वह क्रमशः घटता चला जाता है। यह घटोत्तरी ही अन्ततः हमारी मृत्यु का कारण बनती है। संचित कोश समाप्त होने पर ही मृत्यु होती है।
30 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की अवधि में हमारी मांसपेशियों का भार लगभग एक तिहाई कम हो जाता है। उसी अनुपात से शक्ति घटती चलती है। इस बीच तीन चौथाई तंत्रिका तंतु समाप्त हो जाते हैं और एक चौथाई ही बचते हैं। इसलिये मस्तिष्क का शरीर पर उतना नियन्त्रण नहीं रह जाता, जितना आवश्यक है। दिमाग एक तिहाई खराब हो जाता है। उसका वजन 3.03 पौण्ड से घटकर 2.22 पौण्ड ही रह जाता है। गुर्दों में मूत्र साफ करने वाले ‘नेफोन’ घटकर आधे रह जाते हैं जिससे वह पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और रक्त में उस अशुद्धता की मात्रा बढ़ती जाती है। काम करते थक और घिस जाने के कारण ज्ञानेन्द्रियां अपना आवश्यक उत्तरदायित्व वहन नहीं कर पातीं, उन्हें पोषक तत्व भी शुद्ध तथा उपयुक्त मात्रा में मिल नहीं पाते, इसलिये उनकी घिसट की क्षति पूर्ति भी नहीं हो पाती।
25 साल के युवक की तुलना में 80 साल के बूढ़े का दिल प्रायः आधी मात्रा में खून पम्प कर पाता है। यही हालत फेफड़ों की होती है, सांस की सफाई करने में वे अपनी ड्यूटी आधी ही दें पाते हैं। तन्त्रिका तन्तुओं में विद्युत आवेग की दौड़ 20 प्रतिशत शिथिल हो जाती है इसलिए शरीर द्वारा मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने में और वहां का सन्देश अंगों के लिए लाने में देर लग जाती है। स्थिति के अनुरूप तुरंत निर्णय लेने या कदम उठाने में बुढ़ापा धीरे-धीरे शिथिलता ही उत्पन्न करता चला जाता है। यही सब कारण हैं जिनसे हम ढलती आयु में क्रमशः मृत्यु के निकट घिसटते चले जाते हैं। शक्ति की कमी, कल पुर्जों का घिस जाना, संचित पूंजी का खर्च, नये उत्पादन में शिथिलता एवं मलों का बढ़ते जाना शरीर के लिए मरण ही प्रस्तुत करेगा। बुढ़ापा जीवन को मृत्यु के पथ पर धकेलने ले चलने वाली एक ऐसी निर्मम प्रक्रिया है जिससे बच सकना कठिन दीखता है। बुढ़ापा न टला तो मृत्यु कैसे टलेगी। दोनों एक दूसरे के सगे सहोदर जो हैं।
कोशिकाओं में चलती रहने वाली रासायनिक क्रिया में विषाक्त पदार्थों का अनुपात बढ़ते जाने और प्रोटीन का चालीस प्रतिशत भाग कोलाजेन में बदल जाने से जीवन संकट बढ़ाता ही जाता है। त्वचा के नीचे का कोलाजन कठोर होता जाता है। फलस्वरूप चमड़ी पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। दांतों का गिरना, बालों का झड़ना यह प्रकट करता है कि भीतर की पकड़ ढीली होती जा रही है।
शारीरिक और मानसिक शक्तियों के अनावश्यक अपव्यय को रोकने के लिए सीधा, सरल, सौम्य और हलका फुलका जीवन जिया जाना चाहिए इसके लिए पौष्टिक औषधियों की तलाश बेकार है। सबसे बड़ी औषधि एक ही है कि जीवन को भारी, बोझिल और कृत्रिम न बनने दिया जाय। अपव्यय को रोका जा सका तो लम्बे समय तक युवावस्था को भी सुरक्षित बनाये रखा जा सकता है।
केवल दीर्घ जीवन ही सम्भव नहीं वरन् यह भी सम्भव है कि ढलती आयु में भी सशक्त यौवन को स्थिर रखा जा सके। शरीर में आयु की वृद्धि के साथ कुछ तो परिवर्तन होते हैं पर यह मानवी प्रयत्नों पर निर्भर है कि वह शिथिलता से अपने को बचाये रहें और वृद्ध होते हुए भी अशक्त न बनें।
वारजन विवारेस नियासी पियर डिफोरवेल 129 वर्ष का होकर सन् 1809 तक जीवित रहा। मरते समय उसका स्वास्थ्य ठीक था और उसकी सभी इन्द्रियां अपना काम ठीक तरह करती थीं। उसने तीन विवाह किये और कितने ही बच्चे पैदा हुए उनमें से तीन बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें तीन पृथक शताब्दियों में पैदा हुआ कहा जाता है। एक बच्चा 1699 में दूसरा 1738 में तीसरा 1801 में जन्मा। यों यह अन्तर लगभग सौ वर्ष ही होता है पर शताब्दियों के हिसाब से इसे तीन शताब्दियों में भी गिना जा सकता है और साहित्यिक शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि उसका एक बच्चा 16वीं शताब्दी में, दूसरा 17वीं में और तीसरा अठारहवीं में जन्मा। उसकी तीसरी पत्नी 19 वर्ष की थी जबकि डिफोरवेल 120 वर्ष का। यह तीसरा दाम्पत्य जीवन भी उसने प्रसन्नता पूर्वक बिताया। पत्नी को इसमें कोई कमी दिखाई न दी। यह विवाह नौ वर्ष तक सुखपूर्वक चला और उसमें कई बच्चे हुए।
उपरोक्त तीन शताब्दियों में जन्मे तीन बच्चों की जन्म तिथियां उनके प्रमाण पत्रों समेत सन् 1877 के ‘मेगासिन पिटारेस्क’ में छपी हैं। जो घटना क्रम की यथार्थता प्रकट करते हुए यह भी सिद्ध करती हैं कि दीर्घ जीवन ही नहीं यौवन को भी अक्षुण्य बनाये रहना सम्भव है—असम्भव नहीं।
बहुत दिन से यह सोचा जा रहा है कि आयुवृद्धि के साथ-साथ हारमोन उत्पादन में जो असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है उसकी पूर्ति कर देने से सम्भवतः शरीर की क्षरण प्रक्रिया रुक सकती है और अधिक समय तक जिया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रयोग और परीक्षण भी चले हैं। ब्रिटेन के विज्ञानी सर विन्सेण्ट विगल वथ ने रोडस नामक एक छोटे कीड़े पर यह प्रयोग किया। उन्होंने उसी जाति के एक युवा कीड़े की एक्डायो सोन हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रन्थि एक दूसरे बूढ़े कीड़े के शरीर में लगा दी। इससे उसका बुढ़ापा रुक गया। जब भी शिथिलता के लक्षण दिखाई पड़ते तभी नई ग्रन्थि लगा दी जाती, इस प्रकार उसकी वृद्धि और जवानी का क्रम काफी लम्बे समय तक बनाये रखने में सफलता पाई गई।
मनुष्य शरीर में आयु वृद्धि के साथ घटने वाले एक हारमोन समूह को ‘स्टोरोइड’ कहते हैं। इसकी क्षति पूर्ति अन्यत्र से की जाय तो सम्भव है मनुष्य की जवानी बनी रहे। इसी प्रकार ‘टेस्टोस्टेरीन’ हार्मोन का किसी प्रकार प्रवेश अथवा परिवर्धन किया जा सके तो आदमी जवान बना रह सकता है। इन सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरह-तरह के अनुसन्धान कर रहे हैं।
वैज्ञानिक एक प्राणी की हार्मोन ग्रन्थियां दूसरे के लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका प्रभाव स्वल्प कालीन होता है। यौवन को अक्षुण्य बनाये रहने वाले हार्मोन बिना एक दूसरे के अंग प्रत्यारोपण के भी विकसित किये जा सकते हैं। इसके लिए योगाभ्यास की वही परिपाटी उपयुक्त है जिसे ऋषि-महर्षि कायाकल्प के नाम से प्रयोग करते थे और शताब्दियों तक जीवित रहते थे।
लोक मान्यताओं की बात दूसरी है, पर विज्ञान के लिए यह प्रश्न काफी जटिल है। परमाणुओं की तरह जीवाणु भी अमरता के सन्निकट ही माने जाते हैं। जीवाणुओं की संरचना ऐसी है जो अपना प्रजनन और परिवर्तन क्रम चलाते हुये मूलसत्ता की अक्षुण्ण बनाये रहती है। जब मूल इकाई अमर है तो उसका समुदाय-शरीर क्यों मर जाता है? उलट-पुलटकर वह जीवित स्थिति में ही क्यों नहीं बना रहता? उनके बीच जब परस्पर सघनता बनाये रहने वाली चुम्बकीय क्षमता का अविरल स्रोत विद्यमान है तो कोशाओं के विसंगठित होने और बिखरने का क्या कारण है? थकान से गहरी नींद आने और नींद पूरी होने पर फिर जग पड़ने की तरह ही मरना और मरने के बाद फिर जी उठना क्यों सम्भव नहीं हो सकता?
बैक्टीरिया से लेकर अमीबा तक के दृश्यमान और अदृश्य जीवधारी अपने ही शरीर की उत्क्रान्ति करते हुए अपनी ही परिधि में जन्म-मरण का चक्र चलाते हुए प्रत्यक्षतः अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रहते हैं। फिर बड़े प्राणी ही क्यों मरते हैं? मनुष्य को ही क्यों मौत के मुंह में जाने के लिए विवश होना पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर में जर्मनी के जीव विज्ञानी आगस्ट वीजमान का कथन है कि जीव विकास की प्रगति श्रृंखला में प्राणियों का मरण तब से प्रारम्भ हुआ जब उनमें मेरुदण्ड और मस्तिष्क का विकास, विस्तार आरम्भ होने लगा। मेरुदण्ड भी वस्तुतः मस्तिष्क का ही एक पूंछ जैसा भाग है। मरण को कभी नाड़ी या हृदय की धड़कन के साथ जोड़ा जाता था, पर अब जीवन सत्ता में प्रधानता मस्तिष्क की ही मानी जाती है। हृदय समेत अन्य अवयव उसी के आज्ञानुवर्ती माने जाते हैं। अन्य अवयवों के निःचेष्ट हो जाने पर भी यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की हलचल विद्यमान है तो प्रत्यक्षतः उसे मृतक घोषित किये जाने पर भी उसमें जीवन का अस्तित्व माना जाता है और पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जाता है। मरने वालों में से बहुत से घोषित मृत्यु के दस मिनट पश्चात तक मस्तिष्कीय दृष्टि में जीवित पाये गये हैं और कृत्रिम धड़कन एवं श्वास-प्रश्वास की व्यवस्था करके प्राण लौटाने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। इनमें से कितनों को ही जीवित करने में सफलता भी मिल गई है।
मृत्यु भी प्रगतिक्रम की एक सीढ़ी कही जा सकती है। जड़ता में स्थायित्व है। परमाणु और तरंगों की सत्ता में ऊर्जा और हलचल तो है, पर मरण नहीं है। आरम्भिक स्तर के जीवधारियों में भी मरण संकट नहीं है। जीवाणुओं से लेकर एकेन्द्रिय जीवों तक अपनी सत्ता बनाये रहते हैं यों मरण का क्रम तो चलता रहता है, पर इससे उनके अस्तित्व के लिये चुनौती उत्पन्न नहीं होती। वे बिना टकराये और बिना किसी महत्वाकांक्षा के प्रकृति के प्रवाह क्रम में बहते रहते हैं। महत्वकांक्षाएं जहां प्रगति में सहायक हैं वहां उनमें यह खतरा भी मौजूद है कि प्रकृति ऐसे प्राणियों को अपनी सुव्यवस्था में बाधक समझें और उन्हें जल्दी ही अपना बिस्तर गोल करने के लिए रास्ता साफ करती है। मनुष्य के लिये मृत्यु संकट सम्भवतः इसीलिये अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक जटिल और कष्टकर बन गया है।
बीमारियों से मनुष्य का घिरा रहना भी उसका प्रकृति को चुनौती देने का ही दण्ड दुष्परिणाम है। उपभोग की मर्यादाओं का उल्लंघन शरीर संरचना के अनुरूप आचार संहिता न अपनाने से स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है और उसकी दुःखद प्रतिक्रिया आये दिन बीमार रहने के रूप में भुगतनी पड़ती है। जितना सरल, सौम्य, हलका और आवेश उत्तेजनाओं से रहित जीवन जिया जायगा उतना ही मृत्यु का भय और कष्ट हलका होता जायगा।
मौत भयानक या अवांछनीय ही हो, ऐसी बात नहीं। कई बार तो वह जीवन से भी अधिक मूल्यवान, सुखद और सत्परिणाम उत्पन्न करने वाली होती है। देश की सुरक्षा के लिये युद्ध क्षेत्र में जाने वालों में से कितनों को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है और वे उच्च आदर्शों के लिए इस प्रकार गंवाते हुये गर्व गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी इस वीरगति के लिये लोक श्रद्धा भी बरसती है। लोकहित के लिये प्रयत्नशील महानभावों में से कितनों को ही कठिनाइयों से जूझते हुये अकाल मृत्यु का ग्रास होना पड़ता है। कितने ईसा, सुकरात, गान्धी आदि की तरह प्रति पक्षियों द्वारा मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। गीता कहती है कि ऐसा मरण भाग्यवानों को ही उपलब्ध होता है। क्षत्रि धर्म में अनीति से संघर्ष करते हुये मिलने वाले मरण को यश और स्वर्ग देने वाला कहा गया है। मौत यदि बुरी ही होती तो उसे हर कोई कष्टकर ही अनुभव करता। तब गोली और फांसी के सामने दौड़ते हुये चले जाने के लिये कोई तैयार ही न होता वीर बलिदानियों की परम्परा ही समाप्त हो जाती।
कई बार तो जीवन और मौत के बीच कौन सुखद है यह चुनने में मनुष्य को मौत के पक्ष में अपना निर्णय देना पड़ता है। आत्महत्याएं उसी प्रकार के निर्णय का परिणाम होती हैं। समाज उसे किस दृष्टि से देखता है और कानून उसे कितना अवांछनीय दण्डनीय मानता है यह दूसरी बात है, पर जो इस प्रकार के भयानक निर्णय करते हैं और जिन्दगी से मौत को वरिष्ठ मान बैठते हैं उनके अपने भी तो कुछ तर्क होने ही चाहिये। भले ही उन्हें जन विवेक मान्यता न देता हो।
मनोविज्ञान शास्त्र को सुव्यवस्थित बनाने वाले डा. सिंग फ्रायड का नाम विश्व विख्यात है। उनकी समझदारी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हें जबड़े का कैन्सर हो गया था। यह लगातार 16 वर्ष तक चला। इतने समय में उस फोड़े का 33 बार आपरेशन हुआ। फिर भी वे उस असह्य पीड़ा से छुटकारा न पा सके। फलतः उन्होंने मार्फीन की सुई लगा ली और 83 वर्ष की आयु में स्वेच्छामरण को गौरवास्पद मानते हुये विदा हो गये।
इसी प्रकार एक असह्य पीड़ा से छटपटाते हुये असाध्य रोगी की दया भिक्षा स्वीकार करते हुये डा. विन्सेट मान्ट मेरिनो ने स्वेच्छामरण में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध करा दी थी, रोगी को पांच मिनट के भीतर ही चिरशान्ति का लाभ मिल गया। पर कानून ने इसे अपराध ही माना और चिकित्सक को न्यायालय का निर्धारित दण्ड भुगतना पड़ा। महात्मा गांधी ने भी साबरमती आश्रम में एक मृत्यु से छटपटाते हुये बछड़े को मरण की सुई लगाने की आज्ञा दें दी थी और उन्हें तीखे जनविरोध का सामना करना पड़ा था।
यहां स्वेच्छामरण के कानूनी और औचित्य पथ पर चर्चा नहीं हो रही है। देखा यह जा रहा है कि क्या कोई ऐसा भी समय आ सकता है जब जीवन से मरण को अधिक उपयुक्त माना जाय? मृत्यु दण्ड के अपराधियों के लिये भी न्याय परम्परा यही निर्धारण करती है कि उनके जीवित रहने की अपेक्षा मरण ही श्रेयस्कर है।
प्रसंग जीवन और मरण में से वरिष्ठता किसे दी जाय यह निर्णय करने का है। यहां सब कुछ सापेक्ष ही ठहरता है। उपयोगिता ही प्रधान है। न जीवन ही सदा सर्वदा उत्तम समझा जा सकता है और न मृत्यु को ही सर्वथा हेय ठहराया जा सकता है। दोनों ही अपने-अपने स्थान पर गुण-दोष की कसौटी पर कसे जाने के उपरान्त श्रेष्ठ समझे जा सकते हैं।
प्राणियों को इस मनःस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुये महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं—
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरम् । अन्ये स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम् ।।
अर्थात्—प्राणियों को निरन्तर मृत्यु मुख में जाते हुये आंखों से देखते हुये भी लोग अपनी स्थिरता का भ्रम पाल लेते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है?
इस विस्मरण के कारण मृत्यु का नाम सुनते ही साधारण व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। और एक क्षण के लिये वह जैसे मर सा जाता है। मृत्यु से डरने का मानव का स्वभाव सा बन गया है। साधारण सा रोग, मामूली सी घटना, शत्रु का विचार आदि शंका जनक संयोग आते ही कमजोर आदमी कांप उठता है और सोचने लगता है कि कहीं यह बीमारी हमारे प्राण न ले ले। कहीं वह शत्रु हमें मार डालने की न सोच रहा हो। सम्भव है वहां जाने से हम किसी घातक घटना के शिकार बन जायें मृत्यु के भय से मनुष्य खाने-पीने और प्रतिकूलताओं से जमकर मोर्चा लेने से डरता रहता है।
यही नहीं, किसी की मृत्यु देखकर, किसी दुर्घटना का समाचार सुनकर भी अपनी मृत्यु की शंका से आक्रांत हो जाता है। यहां तक कभी-कभी स्वयं भी अकेले में संसार की नश्वरता का विचार आते अथवा अपनी आयु के बीत गये वर्षों पर विचार करने से मृत्यु भय से उद्विग्न हो उठता है। अन्धेरे अथवा अपरिचित स्थानों में निर्भयता पूर्वक पदार्पण करने से भी उसे मृत्यु की शंका निरुत्साहित कर देती है। निःसन्देह मृत्यु का भय बड़ा ही व्यापक तथा चिरस्थायी होता है।
किन्तु, यदि इस मृत्यु भय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये तो यह बड़ा ही क्षुद्र तथा उपहासास्पद ही प्रतीत होगा। पहले तो जो अनिवार्य है अवश्यम्भावी है उसके विषम विषय में डरना क्या? जब मृत्यु अटल है और एक दिन सभी को मरना ही है तब उसके विषय में शंका का क्या प्रयोजन हो सकता है? यह बात किसी प्रकार भी समझ में न आने लायक नहीं है। हमारे पूर्वजों की एक लम्बी परम्परा मृत्यु के मुख में चली जा चुकी है और आगे भी आने वाली प्रजा उनका अनुसरण करती ही जायेगी तब बीच में हमें क्या अधिकार रह जाता है कि उस निश्चित नियति के प्रति भयाकुल अथवा शंकाकुल होते रहें। मृत्यु को यदि जीवन का अन्तिम एवं अपरिहार्य अतिथि मानकर उसकी ओर से निश्चिंत हो जायें तो न जाने अन्य कितने भयों से हम अनायास ही मुक्ति पा जाएं।
आवश्यकता मृत्यु से डरने की नहीं है और न ही उस अनिवार्य वास्तविकता की उपेक्षा करने की है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसलिये तो उसकी चिन्ता कर्म है जो निश्चित है, उसकी चिन्ता कैसी? उसके प्रति तो निश्चित ही रहना चाहिये। हां उसकी निश्चितता का स्मरण सदैव रखना चाहिये। मृत्यु से न तो डरें और न ही उसे भूलने की कोशिश करें। अपितु मृत्यु को जानें, समझें और स्मरण रखें। साथ ही जीवन को भी जानें तथा स्मरण रखें। अधिकांश लोग न तो जीवन की भव्यता का स्मरण रख पाते, न ही मृत्यु के गौरव को समझ पाते। मृत्यु अनायास आने वाली एक निश्चित घटना है और जीवन अनवरत बहने वाला एक अनन्त चेतना-प्रवाह है, ये दोनों ही तथ्य सदा स्मरण रखने योग्य हैं।
शरीर क्षय की आंतरिक क्रियाएं
शरीर-रचना जिन सूक्ष्म परमाणुओं से हुई है, उन्हें ‘जीव-कोश’ कहते हैं। जीव-कोशों से भरा हुआ कलल जीवन-रस (प्रोटोप्लाज्म) कहलाता है यह रस तेईस मौलिक तत्वों से बना है। इसी को जीवन का मूल आधार समझना चाहिये। मोटे तौर पर यह तत्व आहार से मिलते हैं। पर यह प्रतिपादन भी अपूर्ण है। क्योंकि जो तत्व आहार में होते ही नहीं, वे फिर जीवन-रस को कैसे प्राप्त होंगे? आश्चर्य यह है कि वे सभी तत्व जीवन-रस को उपलब्ध होते रहते हैं। भले ही आहार में उनका अभाव रहता हो।
जीव-कोश बढ़ते हैं और फिर एक से दो होते रहते हैं। जब तक यह वृद्धि एवं उत्पत्ति का क्रम चलता रहेगा, तब तक शरीर भी बढ़ता रहेगा। यह वृद्धि-उत्पत्ति रुकते ही शरीर की अभिवृद्धि भी रुक जाती है। इस प्रक्रिया में जब निर्बलता या गड़बड़ी उत्पन्न होती है, तो उसी क्रम से शरीर भी कमजोर या बीमार पड़ता है। अन्तरंग कोशीय जीवन पर ही बाह्य जीवन-मरण निर्भर है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, अवयवों की थकान, घिसट या विकृति भी बढ़ती है, इसका प्रभाव कोषों पर पड़ता है उनकी बाहरी शकल तो यथावत बनी रहती है पर भीतर का ‘जीवन रस’ घटता और सूखता जाता है, उसकी ताजगी और सशक्तता भी घट जाती है, यही बुढ़ापे का कारण है। जब जीवन रस अधिक घट जाता है या निकम्मा हो जाता है तो जीव कोश मरने लगते हैं यही मृत्यु का कारण है। देर में या जल्दी जब भी मौत होगी—किसी भी कारण से होगी शरीर के भीतर यही स्थिति पाई जायगी।
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर कानूनगो के नेतृत्व में इस प्रकार के अध्ययन के लिए एक टोली नियुक्त की थी कि बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार बताये जाने वाले एंजाइमों, हारमोनों, ऊतकों, कोशिकाओं, रासायनिक तत्वों एवं मनोभावों का इस संदर्भ में कितना हाथ है। अध्ययन से पता चला—
(1) देखा गया है कि आयु वृद्धि के साथ-साथ उपापचयन एवं न्यूरोह्यू मोरल नियमन प्रणाली में परिवर्तन होने लगता है और कोमलता का स्थान कठोरता लेने लगती है यहीं से बुढ़ापा प्रारम्भ होता है। बालक की कोमलता किशोर अवस्था में घट जाती है और वह अपेक्षाकृत कठोर दीखने लगता है यह बुढ़ापे का ही प्रारम्भिक रूप है। (2) आनुवांशकी सिद्धान्त के अनुसार पैन्टक जीन्स भी अल्पायु दीर्घायु जरायुक्त यौवन, और यौवन युक्त जरा के लिए जिम्मेदार हैं। माता से 23 और पिता से 23 इस प्रकार 46 गुणसूत्रों में जुड़े हुए असंख्य ‘जीन्स’ शरीर में विद्यमान रहते हैं। इनमें भी वे बीज विद्यमान रहते हैं जो जवानी को देर तक बनाये रहें अथवा नई उम्र में ही बुढ़ापा खड़ा कर दें।
(3) संयोजी ऊतक हमारे सारे शरीर में फैले हैं। उनकी संख्या हड्डियों के सिरों से जुड़ी हुई मांस पेशियों में सबसे अधिक होती है। यह जोड़ ही हड्डियों का नियन्त्रण करते हैं। इन संयोजी ऊतकों में तीन अघुलनशील प्रोटीनें पाई जाती हैं। (1) कोलाजेन (2) इलास्टिन (3) रेडिक्रलित। इनमें से कोलाजेन शरीर का एक तिहाई भाग बनाती है और कोशिकाओं के बीच जोड़ का काम करती है। यह उपयोगिता होते हुए भी जब उसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो अमिनो अम्ल उभरता है और शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। (4) हमारे शरीर में प्रतिदिन अगणित कोशिकायें जन्मती और मरती हैं। किन्तु मस्तिष्क की तांत्रिक कोशिकाओं के बारे में यह बात नहीं है। उनका पुनर्निर्माण नहीं होता। मस्तिष्क में कोशिकायें प्रति घन सेन्टी मी. एक करोड़ के अनुपात में पाई जाती हैं। वे प्रति घण्टे एक हजार की औसत से मरती रहती हैं। इस प्रकार यह पूंजी क्रमशः घटती रहती है। बहुधा जीवन-काल में ही 10 प्रतिशत मस्तिष्क घट जाता है। यह पूंजी समाप्त होते चलने से शरीर पर मनःचेतना का नियन्त्रण घटता चलता है और वह कभी बुढ़ापे का निमित्त बन जाती है।
(5) हृदय, शिरायें, पेशियां, ग्रन्थियां, तांत्रिकी मृच्छिकायें जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को समर्थ बनाये रखने वाले रासायनिक पदार्थ घट जाते हैं। आयुवृद्धि के साथ-साथ रड्रिनेलिन, थायरोक्शिन, कोर्टिसोन, डिसौक्सीकौटिंकोटरीन इन्सुलीन, सैक्स हारमोनों जैसे तत्वों की कमी होने से वे अंग शिथिल पड़ जाते हैं। मस्तिष्क के अधः चेतन भाग हाईपोथेलेमस—का नियन्त्रण ढीला हो जाता है और यह बिखराव बुढ़ापे के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्कीय विद्युत तरंगें—अल्फा वेव—तब मन्द हो जाती हैं और बाल सफेद होने लगते हैं।
(6) डी.एन.ए. अणु शरीर की प्रोटीनों का ढांचा बनाता है। वह आयुवृद्धि के साथ-साथ भटकना शुरू करता है फलस्वरूप प्रोटीन वायोसिथेसिस प्रणाली लड़खड़ाने लगती है और बुढ़ापा आ घेरता है।
सोचा यह जा रहा है कि उपरोक्त अवरोधों को देर तक शरीर तन्त्र में प्रविष्ट न होने से रोकने के लिए क्या उपाय अपनाये जायं। रहन-सहन की आहार-विहार की क्या पद्धति निर्धारित की जाय ताकि विकृतियों का क्रम न्यूनतम बना रहे और यौवन की स्थिरता देर तक बनी रहे।
जीन फिनोल ने अपनी पुस्तक ‘दि फिलोसोफी आफ लोंग लाइफ’ में लिखा है—‘मृत्यु की दिशा में आधी यात्रा हम स्वाभाविक रीति से करते हैं और आधी अस्वाभाविक रीति से। स्वाभाविक वह है जिसमें एक नियत क्रम से वृद्धावस्था आती है और परिपक्व आयु भोगकर शरीर असमय बुढ़ापा हमीं बुलाते हैं। मृत्यु की गोद में चला जाता है, अस्वाभाविक वह जिसमें मनुष्य छोटी-मोटी बीमारियों के समय—बढ़ती आयु का लेखा-जोखा रखते हुए—अपनी आयु के मरने वालों की लिस्ट बनाकर यह सोचता रहता है कि अब मृत्यु का समय नजदीक आ गया। यह मान्यता यों महत्वहीन मालूम पड़ती है, पर सच्चाई यह है कि वह अन्तर्मन में एक सुनिश्चित संकल्प बनकर बैठ जाती है और मृत्यु को जल्दी ही कहीं से पकड़ कर ले आती है। संकल्पों से परिस्थितियों का उत्पादन एक सुनिश्चित सत्य है अतएव समय से पूर्व अस्वाभाविक मृत्यु के मुख में चला जाना भी एक यथार्थता ही है।
वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार मनुष्य एक अग्नि पिण्ड की तरह—जलते हुए दीपक की तरह है। आग ऑक्सीजन खाती है और कार्बन डायऑक्साइड गैस उगलती है। बिलकुल यही क्रम मनुष्य का भी है। उसकी श्वास प्रश्वांस क्रिया इसी क्रिया को सम्पन्न करती है। हमारा शरीर—जीवन की एक दिव्य अग्नि की तरह ही ज्वलन्त है। इस भट्टी में यदि उपयुक्त ईंधन पड़ता रहे और उन कारणों से बचा जा सके जो उसे ठण्डी कर देते हैं तो फिर मरने में आमतौर से जो उतावली हो जाती है वह न हो और देर तक जीवित रह सकना संभव हो जाय।
देर तक जीवित रह सकने के महत्वपूर्ण आधार जिन्दगी के साथ जुड़े हुये हैं, यदि उन्हें ठीक तरह संभाले, संजोये रखा जा सके। उद्धत आचरण और उच्छृंखल विचारों से बचा जा सके तो न केवल देर तक वरन् सुख पूर्वक जीवित रहने का आनन्द बिना किसी अड़चन के लिया जा सकता है। मौत के समीप लाने वाले कारण यों समय-समय पर सामने आते रहते हैं, पर वे ऐसे नहीं हैं जिन्हें निरस्त न किया जा सके। हम भीतर से हारते हैं तो बाहर से भी पराजय ही आ घेरती है। भीतर से थकते हैं तो चारों ओर से निराशा और असफलता की घटनाएं घिरती चली आती हैं।
असमय मरण और कुछ नहीं हमारी निरन्तर की भूलों का ही दुष्परिणाम है। यदि सतर्कता बरती जाय तो हम शताब्दियों तक जी सकते हैं और अन्तिम सांस तक हंसते-खेलते उल्लासपूर्ण मनःस्थिति में रह सकते हैं। ध्यान यदि आन्तरिक संतुलन का रखा जा सके तो बाहरी क्रिया-कलाप में रहने वालों अवांछनीय भूलें सहज सहज ही घटती और मिटती चली जायेंगी।
बुढ़ापा आयु के आधार पर नहीं विचारों के आधार पर आता है। यदि ऐसा न होता तो तीस वर्ष में लोग बूढ़े और सत्तर वर्ष के जवान क्यों दिखाई पड़ते?
वैज्ञानिक जेक्त लूटो ने कितने ही प्राणियों का शारीरिक तापमान गिराकर उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है और पाया है कि इससे इनका जीवन काल आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। उनका कथन है कि यदि मनुष्य का स्वाभाविक तापमान 98.6 से घटाकर आधा अर्थात् 49.3 किया जा सकें तो आयु 20 गुनी बढ़ सकती है। 70 वर्ष जीने योग्य शरीर को 1400 वर्ष जिन्दा रखा जा सकता है।
मानवी जीवकोशों की सुदृढ़ता को परखते हुए कोलंबिया विश्वविद्यालय के डा. एच.एस. सिक्स ने कहा है यदि स्नायु उत्तेजना और रासायनिक विकृतियों से शरीर की रक्षा की जा सके तो मनुष्य की संरचना उसे 800 वर्ष तक जीवित रहने का अवसर दें सकती है।
कार्नेट विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान ने अपने परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला है कि शारीरिक श्रम की तुलना में नीरस मानसिक श्रम से कहीं अधिक थकान आती है। खाद्य-पदार्थों में पाई जाने वाली ऊष्मा जिसे ‘कैलोरी’ कहते हैं यदि कम मात्रा में मिले तो थकान आवेगी। यह मान्यता भी अभी पूर्णतया निरस्त नहीं हुई है। पिछली शताब्दी के यह निष्कर्ष अभी भी दुहराये जाते हैं कि भोजन में ऊष्मा की मात्रा समुचित हो तो थकान से बचा जा सकता है और बुढ़ापा वस्तुतः थकान ही है। यह माना जाता है कि 150 पौण्ड वजन का कोई व्यक्ति सोते समय 65 कैलोरी प्रति घण्टा खर्च करता है। लेटे रहने में 77, पढ़ने में 100, टाइप करने जैसे कामों में 145, चलने-फिरने में 200 और कड़ा परिश्रम करने में 300 कैलोरी प्रति घण्टा के हिसाब से खर्च होती है।
डा. वाल्डविन के अनुसार मनुष्य शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री रहता है, पर उसे अनुकूल 68 डिग्री तापमान का वातावरण ही पड़ता है। इससे अधिक ठण्डक या गर्मी होने पर उसकी कैलोरी शक्ति अधिक मात्रा में खर्च होने लगती है और थकान जल्दी चढ़ती है। डा. डीनाल्ड ए. लेयर्ड के अनुसार कोलाहल भरे वातावरण में रहने वाले मनुष्य को 20 प्रतिशत थकान उस शोरगुल के कारण ही चढ़ती रहती है।
मेयोक्लीनिक के डा. केन्द्रिल ने कहा है चिड़चिड़ापन मनुष्य की थकान का सर्वविदित चिन्ह है। लेहीक्लीनिक के डा. एलेक का मत भी यही है—वे कहते हैं चिड़चिड़ा मनुष्य दया का पात्र है क्योंकि वस्तुतः वह गहरी थकान का मरीज होता है। उस पर क्रोध करने या बदला लेने से तो इस मरीज का और भी अहित होगा। थकान बढ़ेगी और बुढ़ापे की रफ्तार तेज होगी।
जीव विज्ञानियों के अनुसार मृत्यु एक प्रकार की अत्यधिक गहरी थकान अथवा इतनी प्रगाढ़ निद्रा है जिसमें गिरने के बाद फिर जागृत हो सकना सम्भव नहीं हो पाता। यदि इस थकान को दूर करने जितने समय तक सुरक्षित विश्राम की व्यवस्था बन जाय और जागने की अवधि तक शरीर के जीवाणुओं को मरने, सड़ने या सूखने से बचाया जा सके तो मृत्यु के बाद फिर कुछ समय बाद जी उठना सम्भव हो सकता है।
चेतना मरती नहीं थक जाती है। बुढ़ापे के कारण नाड़ी संस्थान की लचक घट जाती है कोशिकाओं का नवीनीकरण क्रम शिथिल हो जाता है। शरीर यन्त्र उन्हीं कारणों से कठोर एवं शिथिल होता चला जाता है। जीवनी शक्ति का इसी क्रम से ह्रास होता है और धीरे-धीरे बढ़ती हुई जराजीर्ण अवस्था मृत्यु के समीप तक जा पहुंचती है। इस कठोरता एवं शिथिलता की गति जितनी मन्द होगी उतने ही अधिक समय तक जीवित एवं सक्रिय रहा जा सकेगा। थकान धीरे-धीरे पैदा हो दीर्घजीवन का प्रधान सूत्र यही है। प्रगाढ़ विश्राम की सुविधा बीच-बीच में इस प्रकार मिलती रहे कि पिछले दिनों की क्षति को पूरा किया जा सके तो फिर यह सम्भव हो जायगा कि बहुत लम्बे समय तक जीवन बना रहे। हर रात को सोने और हर सवेरे उठने का क्रम एक मध्यावधि मरण एवं पुनर्जीवन हो तो है उसी सामान्य क्रम को विशेष उपचार से दीर्घकालीन बनाया जा सके तो कोशिकाओं पर छाई हुई थकान से उत्पन्न जरठता का निवारण हो सकता है और बूढ़े का फिर से जवान बन सकना शक्य बन सकता है।
तीस वर्ष तक हमारा शरीर निरन्तर बढ़ता है। इसके बाद वह क्रमशः घटता चला जाता है। यह घटोत्तरी ही अन्ततः हमारी मृत्यु का कारण बनती है। संचित कोश समाप्त होने पर ही मृत्यु होती है।
30 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की अवधि में हमारी मांसपेशियों का भार लगभग एक तिहाई कम हो जाता है। उसी अनुपात से शक्ति घटती चलती है। इस बीच तीन चौथाई तंत्रिका तंतु समाप्त हो जाते हैं और एक चौथाई ही बचते हैं। इसलिये मस्तिष्क का शरीर पर उतना नियन्त्रण नहीं रह जाता, जितना आवश्यक है। दिमाग एक तिहाई खराब हो जाता है। उसका वजन 3.03 पौण्ड से घटकर 2.22 पौण्ड ही रह जाता है। गुर्दों में मूत्र साफ करने वाले ‘नेफोन’ घटकर आधे रह जाते हैं जिससे वह पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और रक्त में उस अशुद्धता की मात्रा बढ़ती जाती है। काम करते थक और घिस जाने के कारण ज्ञानेन्द्रियां अपना आवश्यक उत्तरदायित्व वहन नहीं कर पातीं, उन्हें पोषक तत्व भी शुद्ध तथा उपयुक्त मात्रा में मिल नहीं पाते, इसलिये उनकी घिसट की क्षति पूर्ति भी नहीं हो पाती।
25 साल के युवक की तुलना में 80 साल के बूढ़े का दिल प्रायः आधी मात्रा में खून पम्प कर पाता है। यही हालत फेफड़ों की होती है, सांस की सफाई करने में वे अपनी ड्यूटी आधी ही दें पाते हैं। तन्त्रिका तन्तुओं में विद्युत आवेग की दौड़ 20 प्रतिशत शिथिल हो जाती है इसलिए शरीर द्वारा मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने में और वहां का सन्देश अंगों के लिए लाने में देर लग जाती है। स्थिति के अनुरूप तुरंत निर्णय लेने या कदम उठाने में बुढ़ापा धीरे-धीरे शिथिलता ही उत्पन्न करता चला जाता है। यही सब कारण हैं जिनसे हम ढलती आयु में क्रमशः मृत्यु के निकट घिसटते चले जाते हैं। शक्ति की कमी, कल पुर्जों का घिस जाना, संचित पूंजी का खर्च, नये उत्पादन में शिथिलता एवं मलों का बढ़ते जाना शरीर के लिए मरण ही प्रस्तुत करेगा। बुढ़ापा जीवन को मृत्यु के पथ पर धकेलने ले चलने वाली एक ऐसी निर्मम प्रक्रिया है जिससे बच सकना कठिन दीखता है। बुढ़ापा न टला तो मृत्यु कैसे टलेगी। दोनों एक दूसरे के सगे सहोदर जो हैं।
कोशिकाओं में चलती रहने वाली रासायनिक क्रिया में विषाक्त पदार्थों का अनुपात बढ़ते जाने और प्रोटीन का चालीस प्रतिशत भाग कोलाजेन में बदल जाने से जीवन संकट बढ़ाता ही जाता है। त्वचा के नीचे का कोलाजन कठोर होता जाता है। फलस्वरूप चमड़ी पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। दांतों का गिरना, बालों का झड़ना यह प्रकट करता है कि भीतर की पकड़ ढीली होती जा रही है।
शारीरिक और मानसिक शक्तियों के अनावश्यक अपव्यय को रोकने के लिए सीधा, सरल, सौम्य और हलका फुलका जीवन जिया जाना चाहिए इसके लिए पौष्टिक औषधियों की तलाश बेकार है। सबसे बड़ी औषधि एक ही है कि जीवन को भारी, बोझिल और कृत्रिम न बनने दिया जाय। अपव्यय को रोका जा सका तो लम्बे समय तक युवावस्था को भी सुरक्षित बनाये रखा जा सकता है।
केवल दीर्घ जीवन ही सम्भव नहीं वरन् यह भी सम्भव है कि ढलती आयु में भी सशक्त यौवन को स्थिर रखा जा सके। शरीर में आयु की वृद्धि के साथ कुछ तो परिवर्तन होते हैं पर यह मानवी प्रयत्नों पर निर्भर है कि वह शिथिलता से अपने को बचाये रहें और वृद्ध होते हुए भी अशक्त न बनें।
वारजन विवारेस नियासी पियर डिफोरवेल 129 वर्ष का होकर सन् 1809 तक जीवित रहा। मरते समय उसका स्वास्थ्य ठीक था और उसकी सभी इन्द्रियां अपना काम ठीक तरह करती थीं। उसने तीन विवाह किये और कितने ही बच्चे पैदा हुए उनमें से तीन बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें तीन पृथक शताब्दियों में पैदा हुआ कहा जाता है। एक बच्चा 1699 में दूसरा 1738 में तीसरा 1801 में जन्मा। यों यह अन्तर लगभग सौ वर्ष ही होता है पर शताब्दियों के हिसाब से इसे तीन शताब्दियों में भी गिना जा सकता है और साहित्यिक शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि उसका एक बच्चा 16वीं शताब्दी में, दूसरा 17वीं में और तीसरा अठारहवीं में जन्मा। उसकी तीसरी पत्नी 19 वर्ष की थी जबकि डिफोरवेल 120 वर्ष का। यह तीसरा दाम्पत्य जीवन भी उसने प्रसन्नता पूर्वक बिताया। पत्नी को इसमें कोई कमी दिखाई न दी। यह विवाह नौ वर्ष तक सुखपूर्वक चला और उसमें कई बच्चे हुए।
उपरोक्त तीन शताब्दियों में जन्मे तीन बच्चों की जन्म तिथियां उनके प्रमाण पत्रों समेत सन् 1877 के ‘मेगासिन पिटारेस्क’ में छपी हैं। जो घटना क्रम की यथार्थता प्रकट करते हुए यह भी सिद्ध करती हैं कि दीर्घ जीवन ही नहीं यौवन को भी अक्षुण्य बनाये रहना सम्भव है—असम्भव नहीं।
बहुत दिन से यह सोचा जा रहा है कि आयुवृद्धि के साथ-साथ हारमोन उत्पादन में जो असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है उसकी पूर्ति कर देने से सम्भवतः शरीर की क्षरण प्रक्रिया रुक सकती है और अधिक समय तक जिया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रयोग और परीक्षण भी चले हैं। ब्रिटेन के विज्ञानी सर विन्सेण्ट विगल वथ ने रोडस नामक एक छोटे कीड़े पर यह प्रयोग किया। उन्होंने उसी जाति के एक युवा कीड़े की एक्डायो सोन हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रन्थि एक दूसरे बूढ़े कीड़े के शरीर में लगा दी। इससे उसका बुढ़ापा रुक गया। जब भी शिथिलता के लक्षण दिखाई पड़ते तभी नई ग्रन्थि लगा दी जाती, इस प्रकार उसकी वृद्धि और जवानी का क्रम काफी लम्बे समय तक बनाये रखने में सफलता पाई गई।
मनुष्य शरीर में आयु वृद्धि के साथ घटने वाले एक हारमोन समूह को ‘स्टोरोइड’ कहते हैं। इसकी क्षति पूर्ति अन्यत्र से की जाय तो सम्भव है मनुष्य की जवानी बनी रहे। इसी प्रकार ‘टेस्टोस्टेरीन’ हार्मोन का किसी प्रकार प्रवेश अथवा परिवर्धन किया जा सके तो आदमी जवान बना रह सकता है। इन सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरह-तरह के अनुसन्धान कर रहे हैं।
वैज्ञानिक एक प्राणी की हार्मोन ग्रन्थियां दूसरे के लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका प्रभाव स्वल्प कालीन होता है। यौवन को अक्षुण्य बनाये रहने वाले हार्मोन बिना एक दूसरे के अंग प्रत्यारोपण के भी विकसित किये जा सकते हैं। इसके लिए योगाभ्यास की वही परिपाटी उपयुक्त है जिसे ऋषि-महर्षि कायाकल्प के नाम से प्रयोग करते थे और शताब्दियों तक जीवित रहते थे।
Write Your Comments Here:
- धीरे-धीरे आती जाती मृत्यु समीप
- मृत्यु की मीठी गहरी नींद जरूरी
- अर्धमृत न रहें, पूर्ण जीवित बनें
- मरण सृजन का अभिनव पर्व—उल्लासप्रद उत्सव
- आसक्ति मनुष्य को मृत्यु के बाद भी घुमाती है
- मृतात्मा को क्षुब्ध नहीं, तृप्त करें
- सुदीर्घ विश्राम की अवधि को सार्थक बनाएं
- पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को क्रिया से जोड़ें