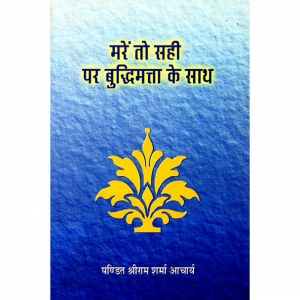मरे तो सही, पर बुद्धिमत्ता के साथ 
मृतात्मा को क्षुब्ध नहीं, तृप्त करें
Read Scan Version
मृत्यु के समय परिजनों का भी यह कर्त्तव्य होता है कि वे ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि मरणशील व्यक्ति आनन्द और प्रसन्नता के साथ अपनी अगली यात्रा पर जा सके। उस समय रामचरितमानस, गीता, जपुजी, उपनिषद् आदि का पाठ करने, भजन कीर्तन करने की परम्परा उचित एवं आवश्यक है। चारों ओर शांति तथा वैराग्य का वातावरण रहने पर मरणशील व्यक्ति के भी वैसे ही संस्कार जागृत-सक्रिय हो उठते हैं और वह शान्ति के साथ शरीर छोड़कर गन्तव्य की ओर प्रस्थान करता है।
न केवल मृत्यु के तत्काल बाद भी पूर्व, अपितु मृत्यु के तत्काल बाद भी शांति तथा वैराग्य का ही वातावरण बनाए रखना चाहिए। उस समय रोना-धोना, चीखना-चिल्लाना, छाती पीटना, आर्तनाद करना--विलाप के साथ आसक्ति-उत्प्रेरक घटनाएं याद करना और इसी प्रकार की अन्य चेष्टाएं अनुचित हैं। उससे मृत व्यक्ति की आत्मा को क्लेश ही होगा।
यों भी सामान्यतः व्यक्ति के संस्कार मरणोपरांत खींच-खींचकर उसे घर की ओर ले आते हैं। स्थूल शरीर से मुक्त जीवात्मा का सूक्ष्म-शरीर देर तक घर में ही मंडराता रहता है अतः उस समय रोना-धोना नहीं चाहिए। अन्यथा शरीर-मुक्त जीवात्मा को कष्ट होगा। सिंधी लोगों में तथा कुछ अन्य समाजों में उस समय भजन-कीर्तन की परम्परा है, जो अत्युत्तम है। वे क्षण शोक-विलाप के नहीं भावभरी श्रद्धांजलि के होते हैं। प्रभु से प्रार्थना की जानी चाहिए कि दिवंगत की आत्मा शांति के साथ अगली यात्रा पर जाए और उस नई शक्ति, नई स्फूर्ति तथा आलोकपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो। शोक-संताप से तो उसे कष्ट ही होगा। यात्रा के लिए उसे प्रकाश पूर्ण पाथेय चाहिए शोकांधकार जीवात्मा की अगली यात्रा में पग-पग पर अवरोध ही उपस्थित करेगा।
ईसाइयों में इस सम्बन्ध में एक मार्मिक कहानी प्रचलित है। किसान का बच्चा मर गया। बच्चे से बाप को अत्यधिक मोह था। उसकी मृत्यु ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसका मन कराह उठा। वह दिन−रात टीस और पीड़ा से भरा रहता। उसे जीवन निस्सार और निरानन्द प्रतीत होने लगा। न काम में मन लगता, न आराम ही कर पाता। कई दिन बीत गए। तब एक रात किसान ने एक हृदयस्पर्शी स्वप्न देखा। उसने देखा कि स्वर्गलोक में नन्हे-मुन्ने प्यारे-प्यारे फूल जैसे कोमल, सुन्दर बच्चों का झुंड उल्लास के साथ कोई उत्सव मना रहा है। उसी समारोह में सब बच्चे अपने-अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर पंक्तिबद्ध आगे बढ़ते हैं। मोमबत्तियों का प्रकाश दिव्य और प्रखर तथा अकम्प है। सब बच्चे उस प्रकाश में तेजी से आगे ही बढ़ते जाते हैं। बस एक बच्चा रह-रहकर ठिठक जाता है। उसकी मोमबत्ती बार-बार बुझ जाती है साथी सहयात्री बालक उसे फिर जलाते हैं। वह एक-दो कदम बढ़ता है तभी मोमबत्ती फिर बुझ जाती है। इस क्रम की आवृत्ति बार-बार होती है। लड़का रुआंसा कातर हो उठता है। बूढ़ा किसान दयाभाव से भरकर उधर बढ़ता है तो चौंक उठता है-यह तो उसी का बच्चा है। वह पूछता है—‘बेटे! तुम्हारी ही मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है बार-बार।’ बच्चा उत्तर देता है—‘‘क्या करें पिताजी जैसे ही मेरे साथी मेरी मोमबत्ती जलाते हैं और मैं चलता हूं वैसे ही आपके आंसू मेरी मोमबत्ती पर टपकते हैं और वह बुझ जाती है।’’ कहानी मार्मिक तो है ही यथार्थ भी है। सगे सम्बन्धियों का शोक-संताप परलोक में जीवात्मा को पीड़ा ही पहुंचाता है। परिजनों का करुण विलाप जीवात्मा को क्षुब्ध-अशांत करता है। अतः ऐसा करना अनुचित और अहितकर है। इसके स्थान पर शांति चित्त से भक्तिपूर्ण भाव से, परमपिता परमेश्वर से उस जीवात्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जिसने जन्म लिया है, उसका मरण सुनिश्चित है। सृष्टि का क्रम ही जन्म-मरण की धुरी पर घूम रहा है। इसलिये आत्मीय जनों की मृत्यु पर शोक की कोई आवश्यकता है नहीं। एक पौराणिक आख्यान है कि अपने पुत्र की मृत्यु से दुःख कातर राजा जब राजकाज ही छोड़ बैठे, और ऋषि नारद के बार-बार समझाने-बुझाने पर भी नहीं माने तब उन्होंने उसी पुत्र के द्वारा राजा को शिक्षा दिलाना उपयुक्त समझा। मुनि की दिव्य प्रेरणा एवं शक्ति प्रयोग से राजकुमार उठ बैठा। उसे देखते ही राजा ने ‘‘मेरे लाड़ले’’ कहकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया इस पर राजकुमार ने उन्हें समझाया—‘‘कैसे लाड़ले और कैसे पिता? राजन! भ्रम में मत पड़ो। तुम्हारा पुत्र मर चुका। मेरी वह भूमिका समाप्त हुई। अब मुझे अगले दायित्व निभाने दें। पता नहीं कितने बार आप मेरे बेटे, भाई मित्र, शत्रु आदि रह चुके हैं और कितने ही बार मैं आपका कभी पिता, कभी बन्धु, कभी साथी, कभी प्रतिस्पर्धी-विरोधी रह चुका हूं। यह जन्म-मरण चक्र अनादि है। आप एक ही भूमिका से आसक्त हो गए हैं। एक क्षणिक लहर को ही आपने समुद्र मान लिया है.....आदि। राजकुमार के उपदेशों और स्पष्ट कथनों से राजा का मोह समाप्त हुआ।
गर्भोपनिषद् में बताया गया है कि गर्भावस्था में जीव के अन्तःकरण में पूर्वजन्मों की स्मृतियां जागृत होती हैं और वह कहता है—‘‘पूर्वयोनि सरस्राणि दृष्ट्रा चैव ततो मया, आहारा विविधा भुक्ता पीता नानाविधाः स्तनाः जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः। यन्मया परिजन्स्यार्थेकृतं कर्म शुभाशुभं ।। एकाकी तेन दह्येऽहं गतास्ते फलभोगिनः ।’’
अर्थात् हजारों बार मेरा जन्म हो चुका है, विविध प्रकार के आहार में खा चुका हूं, हजारों माताओं का दूध पी चुका हूं, बार-बार पैदा हुआ हूं और बार-बार मरा हूं। आत्मीयों के लिए शुभ और अशुभ कर्म किए हैं। पर वे तो आज साथ हैं नहीं। साथ हैं मेरे कर्म ही उनका ही। फल मुझे मिल रहा है।
इस प्रकार वस्तुतः आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मात्र शरीर की होती है और वह अटल-अनिवार्य है। उसके लिए दुःख करना व्यर्थ है। क्योंकि उस शरीर की चमड़ी से तो प्यार-सम्बन्ध था नहीं। यदि होता तो चमड़ी अभी भी सामने है। फिर न तो वह दुःख का कारण बनती नहीं उसे जलाने-दफनाने का प्रयास होता। स्नेह-अनुराग तो उस शरीर के माध्यम से अब तक क्रियाशील चैतन्य आत्मा से था। वह आत्मा नष्ट हुई नहीं है। इसलिए शोक-क्लेश का न तो कोई कारण है न ही औचित्य। शरीर को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता और आत्मा की मृत्यु कभी हो नहीं सकती। तब फिर कष्ट और रुदन की क्या बात है?
आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होता है और उसी के साथ मर जाता है यह मान्यता पिछले दिनों पदार्थ विज्ञानियों की रही है वे प्राणी को एक चलने-फिरने और सोचने-बोलने वाला समर्थ पौधा मानते रहे हैं। पौधे के जन्म और मरण के साथ ही उसके अस्तित्व का उदय और अन्त ज्ञानी और विज्ञानी एक समान मानते हैं।
प्रश्न प्राणियों के विशेषतया मनुष्य के सम्बन्ध में उपस्थित होता है क्योंकि उसके समाधान से हमारा सीधा सम्बन्ध है। क्योंकि तब सोचना पड़ेगा कि यदि जीवन शरीर के बाद भी बना रहता है तो शरीर त्याग के बाद उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग, नरक, परलोक के प्रसंग इसी सन्दर्भ में सामने आते हैं। यदि पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की स्थिति का इस जन्म पर और इस जन्म का अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? इतना ही नहीं इस सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकला हो उससे वर्तमान जीवन का उपयोग करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने की बात भी सामने आ खड़ी होती है।
सामान्यतया हम भूतकाल से बहुत कुछ सीखते हैं। याद रखते हैं और भावना पूर्वक उस सब को स्मरण रखते हैं जो हमने खोया या पाया है। वर्तमान में जो कुछ हम हैं वह भूतकाल में रोपे गये वृक्ष के ही फल-फूल हैं। भविष्य में कुछ बनता है वह आज के क्रिया-कलाप का प्रतिफल ही होगा। इन दिनों में जो कुछ करते हैं उसका लाभ तत्काल तो मिलता नहीं—कुछ समय उपरांत ही उसके परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार हमारी समस्त गतिविधियां प्रायः भविष्य निर्माण में ही नियोजित रहती हैं। फिर यदि जीवन मरने के बाद भी बना रहता है तो स्वभावतः उसकी भी चिन्ता करनी पड़ेगी और भविष्य के लिए सुखद अवसर प्राप्त करने की तैयारी को भी महत्व देना होगा। यदि जीवन शरीर के साथ ही समाप्त होता है तो मरणोत्तर जीवन के बारे में चिन्ता या तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तब वर्तमान शरीर के वर्तमान और भविष्य को ही सब कुछ मानकर तदनुरूप जीवन यापन की नीति निर्धारित करनी होगी। दोनों परिस्थितियों में दृष्टिकोण अपनाने और कार्यक्रम निर्धारित करने में भारी अन्तर होगा। आस्तिकों को मरणोत्तर भविष्य निर्माण करने के लिए स्वर्ग मुक्ति-शान्ति, सद्गति की बात सोचनी पड़ती है और इस जीवन में तप, संयम, दान, परमार्थ जैसे धर्मानुष्ठानों को महत्व देना पड़ता है भले ही प्रत्यक्षतः उसमें आर्थिक हानि एवं शारीरिक असुविधाएं ही सहन क्यों न करनी पड़ती हों। इसके विपरीत नास्तिक तात्कालिक आमोद-प्रमोद एवं सुख-साधनों को ही महत्व देते हैं। जब देह भस्मीभूत ही ठहरा और पुनरागमन की सम्भावना नहीं रही तो ‘ऋणं कृत्वा घतं पिवेत्’ की नीति अपनाने में कोई अनौचित्य नहीं कहा जा सकता। जीवन का आदि अन्त शरीर तक ही सीमित है या उसके पश्चात् भी उसका अस्तित्व है, यह मात्र दार्शनिक पहेली नहीं है। उसका आज की गतिविधियों से सीधा सम्बन्ध है। एक निश्चय के उपरान्त एक दिशा में चलना पड़ता है और दूसरा निश्चय होने पर दूसरी दिशा में चलने की आवश्यकता अनुभव की जायगी।
क्या मृत्यु की अनुभूति कभी हो सकती है? इसका उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है। मैं मरने वाला हूं, मर रहा, जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए भी कहने वाला अपने को जीवित ही अनुभव करता है। सपने में अपनी मृत्यु का दृश्य देखा जा सकता है। शरीर अचेतन पड़ा हुआ और स्वजन सम्बन्धी रोते कलपते दिखाई पड़ते हैं। इतने पर भी अपनी सत्ता बनी ही दिखती है। मरण का अनुभव अपने को ही होता रहता है। इससे स्पष्ट है कि अपना मरण स्वीकार करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है।
जिसका जो स्वभाव है वह उसे पसन्द होता है और उसकी पूर्ति में प्रसन्न होता है। मछली का जल जीवन स्वभाव है, मच्छर गन्दगी पसन्द करते हैं और खटमल रक्त पीते हैं। इसमें उन्हें घृणा नहीं प्रसन्नता होती है। आत्मा यदि मरणधर्मा होता तो उसे मरने से तनिक भी डर न लगता। चूंकि वह मरना नहीं चाहता, मृत्यु संकट आने पर उससे बचने का हर सम्भव उपाय करता है। मरने से डरना यह बताता है कि मृत्यु अस्वाभाविक है। जीवात्मा उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यों शरीर मरता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती तो भी उसे न केवल अपनी वरन् अपने शरीर और स्वजनों तक की मृत्यु अनुपयुक्त अप्रिय लगती है। जीवन ही आत्मा का धर्म है। अपना मरण तो होता नहीं है। शरीरों पर पदार्थों के लिए मरण स्वाभाविक होते हुए भी चेतना पर उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। यह सब लक्षण इस बात के हैं कि मानवी सत्ता मरणशील नहीं न उसे मरण से कोई सहानुभूति है।
स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग अस्वाभाविक। स्वस्थ सदैव बने रहने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं। अस्वस्थता थोड़े दिन की भी असह्य होती है। किसी प्रियजन के रोगी होने से चिन्ता होती है उसकी स्थिति तथा वजह पूछने जानने के लिए आतुरता व्यक्त की जाती है किन्तु स्वस्थ रहने पर कोई उसके लिए चिन्ता नहीं करता और न यह पूछता है कि आप स्वस्थ क्यों हैं? इससे स्वाभाविक और अस्वाभाविक होने का परिचय मिलता है। मृत्यु और जीवन के संबन्ध में भी यही बात है। मृत्यु का समाचार पाकर या उसकी सम्भावना विदित होने पर चिन्ता सम्वेदना प्रकट की जाने लगती है, पर जीवित रहने पर ऐसी कोई व्यग्रता कहीं से भी नहीं होती। इससे जीवन की स्वाभाविकता सिद्ध है। अस्वाभाविक तो मरण ही है। जब शरीर तक के मरण में अस्वाभाविकता मानी जाती है तब आत्मा की चेतन सत्ता का मरण स्वीकार करने की बात तो किसी के गले उतरती ही नहीं।
इस संसार में जितना पदार्थ सृष्टि के आरम्भ में था उतना ही अन्त तक रहेगा। उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। ठोस, तरल और वायु भूत इन स्थितियों में वस्तुयें बदलती रहती हैं। पानी तरल है, ठण्डक पड़ने पर बर्फ बन जाता है। गर्मी पड़ने पर भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है फिर बादल या ओस बनकर तरल रूप में दिखाई पड़ता है। यही अदला-बदली वस्तुओं की उत्पत्ति और मृत्यु के रूप में प्रकट-अप्रकट होती रहती है, वस्तुतः कोई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। इस सिद्धांत को रसायन शास्त्र के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। भौतिक विज्ञान में इसी सिद्धांत को ‘तत्व का अनुत्पत्तित्व’—तत्व का अतिनाशित्व शक्ति का परिवर्तन—नाम से प्रतिपादित किया गया है। अध्यात्म शास्त्र में पदार्थ और प्राणी दोनों पर ही इसी तथ्य का समान रूप से कार्यान्वयन प्रतिपादित किया गया है। गीता कहती है—‘नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः ।’ अर्थात् जो नहीं था वह पैदा नहीं होता और जो है उसका नाश नहीं हो सकता। इस प्रतिपादन में पदार्थ की तरह आत्मा की अमरता भी सन्निहित है।
किसी से पूछा जाय कि आप का अस्तित्व इस समय है या नहीं, वह यही है, में ही उत्तर दें सकता है। यदि यह ‘मैं’ इस समय विद्यमान है तो वह पहले भी था और आगे भी बना ही रहेगा। हां, नाम, रूप और स्थान का परिवर्तन प्रकृति के स्वाभाविक क्रम के अनुसार अवश्य होता रहता है। यदि स्थानान्तरण को मृत्यु समझा जाय तब तो बात दूसरी है पर यदि विनाश या समाप्ति के रूप में मरण की व्याख्या की जाती हो वह भौतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों ही दृष्टियों से गलत है। आत्मा का अस्तित्व शरीर की मृत्यु होने के उपरान्त भी बना रहता है। इस तथ्य से वे धर्म भी इनकार नहीं करते जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। उस परलोक का अस्तित्व तो उन्हें भी मान्य है, जिसमें मरने के बाद भी आत्मा किसी न किसी स्थिति में निवास करता रहता है।
साधारणतया जन्म शब्द का अर्थ पैदा होना और मृत्यु का नष्ट एवं समाप्त हो जाना है। यह दो घटनायें समझी जाती हैं। संस्कृति भाषा में ‘जन्म’ और ‘मृत्यु’ शब्दों की व्याख्या व्युत्पत्ति में तथ्य को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। उसमें जन्म का अर्थ प्रकट होना और मृत्यु का देखने योग्य न रहना भर है। इन शब्दों में स्थिति के परिवर्तन भर का संकेत है किसी नवीन उत्पादन या आत्यंतिक विकास का प्रतिपादन नहीं है।
संस्कृत की ‘जनी-प्रादुभावे’ धातु से जन्म शब्द बना है। प्रादुर्भाव का अर्थ है—प्रकटीकरण-आकिजिन। प्रकट होने का तात्पर्य है जो छिपा था उसका सामने आ जाना ‘जन्म’ शब्द का दूसरा पर्यायवाचक है। उत्पत्ति यह शब्द उद्-पद् से मिलकर बना है। जिनका अर्थ है ऊपर आना। इस व्याख्या में भी स्थिति के बदलने भर का संकेत है। जन्म के पर्याय वाचकों में एक और शब्द है—‘सृष्टि’ क्रिएशन। यह शब्द (सृज-विसर्गे) धातु से बना है। जिसका तात्पर्य भी लगभग वैसा ही है जैसा कि जन्म एवं उत्पत्ति का। सृष्टि को बाहर आना-प्रत्यक्ष होना कह सकते हैं। हमारी इन्द्रियों में सब कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं है। वे पंचतत्वों से बनी होने के कारण मात्र किन्हीं वस्तुओं की स्थूल स्थिति को ही देख सकती है। कितनी ही वस्तुओं का अस्तित्व सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से—रेडियो टेलिस्कोपों से एवं अन्यान्य साधनों से जाना जा सकता है आंखें एवं इन्द्रियां तो वायु भूत पदार्थों तक को नहीं देख पातीं, जबकि अन्य इन्द्रियां उनकी उपस्थिति का अनुभव करती हैं। आग पर मिर्च जला देने से वे हवा में उड़ जाती हैं। तब उस वायु भूत मिर्च को आंखें नहीं देखतीं किन्तु नाक गन्ध रूप में उसकी उपस्थिति अनुभव करती है। इसके आगे सूक्ष्मता आने पर वे इन्द्रियों की पकड़ से बाहर हो जाती है तो भी उनका अप्रकट अस्तित्व बना रहता है। पदार्थ और आत्मा दोनों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त एक समान लागू होता है। जन्म का अर्थ नवीन उत्पत्ति नहीं किन्तु अप्रकट का प्रकट भर हो जाना है।
‘मृत्यु’ शब्द का संस्कृत भाषा में जो अर्थ है उससे भी वस्तुस्थिति पर भली प्रकार प्रकाश पड़ता है। मृत्यु के लिए नाश शब्द का प्रयोग होता है। ‘नाश-नश-अदर्शने’ धातु से बना है। जिसका तात्पर्य है—देखने योग्य न रहना। इसमें अस्तित्व के अभाव की बात नहीं कही गई है, मात्र इतना ही संकेत है कि वह पदार्थ दृष्टि पथ से ओझल हो गया। ऐसा तो बच्चे ‘आंख मिचौनी’ खेल में भी करते रहते हैं। बादलों की छाया सूर्य चन्द्र तक को गुप्त प्रकट होने तक के लिए विवश करती रहती है। धूप-छांव की स्थिति को सूर्य चन्द्र की उत्पत्ति या समाप्त तो नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार आत्मा के शरीर धारण करने और चोला उतार देने की स्थिति के सम्बन्ध में समझा जाना चाहिए। इसमें अस्तित्व तो बना ही रहता है। उसकी अमरता में कोई अन्तर नहीं आता।
मौत से न डरने की जरूरत है और न उसके लिए उतावले होने की। शरीर ही बदलते हैं आत्मा के अस्तित्व पर मौत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कपड़े बार-बार बदलने पड़ते हैं पर शरीर वही बना रहता है—शरीर भी कपड़े की तरह बदलते रहते हैं। जीवन ईश्वर के समान ही अनादि और अनन्त है। कोई सत्कर्म किया है तो उसका फल अगले दिन—अगले जनम में मिल सकता है उसमें अधीरता की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध हो गये मरने के दिन आ गये। अब पढ़ कर क्या करेंगे? अब के आरम्भों का अपने को क्या प्रतिफल मिलेगा, इस तरह नहीं सोचा जाना चाहिए। जीवन अनन्त है। भविष्य सुविस्तृत है। रात्रि में विश्राम करना पड़ता है और काम में व्यवधान पड़ता है यह सोचकर बहुत दिन में पूरी होने वाली योजना बनाने में कोई संकोच नहीं करता। फिर हमीं अनन्त जीवन में क्रमिक गति से आत्मोत्कर्ष की—सद्गुणों की—सद्ज्ञान की सम्पदा एकत्रित करने में कटिबद्ध क्यों न रहें?
इन मान्यताओं को अपनाये रहकर हम शरीर की मृत्यु निश्चित मानते हुए भी अजर-अमरों जैसा निश्चिन्त प्रसन्न और योजनाबद्ध प्रगतिशील जीवन जी सकते हैं। साथ ही आत्मीयों की मृत्यु को मात्र शरीर-परिवर्तन समझकर उसके लिए विलाप करने से बचे रह सकते हैं। इससे दिवंगत आत्मीय भी क्षुब्ध-दुःखी होने से बचेंगे। हमारा दिन नहीं शुभचिन्तन ही उन्हें तृप्ति सन्तोष और शक्ति देगा।
मृत्यु जीवन का अन्त नहीं
महान् धर्मात्मा राजा जनश्रुति को जब भोग-विलास से वैराग्य हुआ तो उसने देखा कि अब तो उसका शरीर भी जर्जर हो चुका है। शरीर में तप और साधना की शक्ति भी नहीं रही। जीवन भर अज्ञान में अनेक पाप किये उनका पश्चात्ताप राजा को दलने लगा तो वह महामुनि रैक्य के पास पहुंचे और बोले भगवन् मैं धर्म चित्त हुआ राजा आज जीव भाव से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मुझे बतलाइये मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या मेरी असहाय चेतना भी जन्म मृत्यु के बन्धन से मुक्ति पा सकती है। महामुनि रैक्य ने बताया—राजन्! जब मृत्यु का समय आता है तब सब इन्द्रियों की वृत्ति वाणी में लय हो जाती है। वाणी की वृत्ति मन में और मन की वृत्ति तब प्राण में परिवर्तित हो जाती है। जागृत अवस्था में पांच कर्मेन्द्रियां और पांच ज्ञानेन्द्रियां मन की इच्छाओं पर नाचती थीं पर मृत्यु के समय मन प्राण चेतना के वश में चला जाता है तब प्राण ही जीवन भर की स्थिति के अनुरूप नये निर्माण में जुट जाते हैं वह निर्माण चाहे अच्छा हो या बुरा उसका निर्णय चेतना के शरीर छोड़ते समय ही हो जाता है। जो लोग ईश्वर उपासना, तप, ज्ञान सम्वर्धन और साधना द्वारा अपना मनोबल और आत्म-बल विकसित कर लेते हैं वह अनेक गुणों और संस्कारों से युक्त सुन्दर जीवन पाते हैं और जिनकी इन्द्रियों के प्रति लालसा जागृत बनी रहती है वे उन-उन इच्छाओं की पूर्ति के लिये पुनः कोई शरीर धारण करते हैं। यह पटाक्षेप सनातन काल तक चलते रहते हैं।
उपरोक्त कथन में मृत्यु विज्ञान पर जहां संक्षिप्त शास्त्रीय प्रकाश डाला गया है वहां यह समझाने का प्रयत्न भी है कि एक मृत्यु के बाद मनुष्य का अन्त नहीं हो जाता वरन् उसे अपने कर्मानुसार अन्य जन्म भी धारण करने पड़ते हैं। बार-बार जन्म और बार-बार मृत्यु होती है। जब तक सृष्टि का प्रत्येक जीव पूर्णता नहीं प्राप्त कर लेता यह प्रक्रिया कभी बन्द न होगी।
एक बार बालक नचिकेता को भी ऐसी ही प्रबल जिज्ञासा उठी थी, उसने भी यमाचार्य से ऐसा ही प्रश्न किया था—
ये यंप्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्ये के नत्यमस्तीति चान्ये । एतद्विद्यामनुशिष्ट सत्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ।। —कठ. उप. 1-20
‘‘आचार्यदेव! मरे हुये मनुष्य के विषय में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं, मृत्यु हो जाने पर भी जीव बना रहता है। कुछ कहते हैं, उसका नाश हो जाता है। सो आप मुझे उसका निश्चित निर्णय करके बताइये सत्य क्या है?’’
यमाचार्य ने नचिकेता को तब योगाभ्यास कराया और उसके द्वारा उसने यह जाना कि जीव किस प्रकार मृत्यु के उपरान्त यमलोक, प्रेतलोक, वृक्ष, वनस्पति आदि योनियों, भुवर्लोक आदि में जाता है और वहां की परिस्थितियों का वर्तमान जीवन की तरह उपयोग करता है।
यों भी सामान्यतः व्यक्ति के संस्कार मरणोपरांत खींच-खींचकर उसे घर की ओर ले आते हैं। स्थूल शरीर से मुक्त जीवात्मा का सूक्ष्म-शरीर देर तक घर में ही मंडराता रहता है अतः उस समय रोना-धोना नहीं चाहिए। अन्यथा शरीर-मुक्त जीवात्मा को कष्ट होगा। सिंधी लोगों में तथा कुछ अन्य समाजों में उस समय भजन-कीर्तन की परम्परा है, जो अत्युत्तम है। वे क्षण शोक-विलाप के नहीं भावभरी श्रद्धांजलि के होते हैं। प्रभु से प्रार्थना की जानी चाहिए कि दिवंगत की आत्मा शांति के साथ अगली यात्रा पर जाए और उस नई शक्ति, नई स्फूर्ति तथा आलोकपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो। शोक-संताप से तो उसे कष्ट ही होगा। यात्रा के लिए उसे प्रकाश पूर्ण पाथेय चाहिए शोकांधकार जीवात्मा की अगली यात्रा में पग-पग पर अवरोध ही उपस्थित करेगा।
ईसाइयों में इस सम्बन्ध में एक मार्मिक कहानी प्रचलित है। किसान का बच्चा मर गया। बच्चे से बाप को अत्यधिक मोह था। उसकी मृत्यु ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसका मन कराह उठा। वह दिन−रात टीस और पीड़ा से भरा रहता। उसे जीवन निस्सार और निरानन्द प्रतीत होने लगा। न काम में मन लगता, न आराम ही कर पाता। कई दिन बीत गए। तब एक रात किसान ने एक हृदयस्पर्शी स्वप्न देखा। उसने देखा कि स्वर्गलोक में नन्हे-मुन्ने प्यारे-प्यारे फूल जैसे कोमल, सुन्दर बच्चों का झुंड उल्लास के साथ कोई उत्सव मना रहा है। उसी समारोह में सब बच्चे अपने-अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर पंक्तिबद्ध आगे बढ़ते हैं। मोमबत्तियों का प्रकाश दिव्य और प्रखर तथा अकम्प है। सब बच्चे उस प्रकाश में तेजी से आगे ही बढ़ते जाते हैं। बस एक बच्चा रह-रहकर ठिठक जाता है। उसकी मोमबत्ती बार-बार बुझ जाती है साथी सहयात्री बालक उसे फिर जलाते हैं। वह एक-दो कदम बढ़ता है तभी मोमबत्ती फिर बुझ जाती है। इस क्रम की आवृत्ति बार-बार होती है। लड़का रुआंसा कातर हो उठता है। बूढ़ा किसान दयाभाव से भरकर उधर बढ़ता है तो चौंक उठता है-यह तो उसी का बच्चा है। वह पूछता है—‘बेटे! तुम्हारी ही मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है बार-बार।’ बच्चा उत्तर देता है—‘‘क्या करें पिताजी जैसे ही मेरे साथी मेरी मोमबत्ती जलाते हैं और मैं चलता हूं वैसे ही आपके आंसू मेरी मोमबत्ती पर टपकते हैं और वह बुझ जाती है।’’ कहानी मार्मिक तो है ही यथार्थ भी है। सगे सम्बन्धियों का शोक-संताप परलोक में जीवात्मा को पीड़ा ही पहुंचाता है। परिजनों का करुण विलाप जीवात्मा को क्षुब्ध-अशांत करता है। अतः ऐसा करना अनुचित और अहितकर है। इसके स्थान पर शांति चित्त से भक्तिपूर्ण भाव से, परमपिता परमेश्वर से उस जीवात्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जिसने जन्म लिया है, उसका मरण सुनिश्चित है। सृष्टि का क्रम ही जन्म-मरण की धुरी पर घूम रहा है। इसलिये आत्मीय जनों की मृत्यु पर शोक की कोई आवश्यकता है नहीं। एक पौराणिक आख्यान है कि अपने पुत्र की मृत्यु से दुःख कातर राजा जब राजकाज ही छोड़ बैठे, और ऋषि नारद के बार-बार समझाने-बुझाने पर भी नहीं माने तब उन्होंने उसी पुत्र के द्वारा राजा को शिक्षा दिलाना उपयुक्त समझा। मुनि की दिव्य प्रेरणा एवं शक्ति प्रयोग से राजकुमार उठ बैठा। उसे देखते ही राजा ने ‘‘मेरे लाड़ले’’ कहकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया इस पर राजकुमार ने उन्हें समझाया—‘‘कैसे लाड़ले और कैसे पिता? राजन! भ्रम में मत पड़ो। तुम्हारा पुत्र मर चुका। मेरी वह भूमिका समाप्त हुई। अब मुझे अगले दायित्व निभाने दें। पता नहीं कितने बार आप मेरे बेटे, भाई मित्र, शत्रु आदि रह चुके हैं और कितने ही बार मैं आपका कभी पिता, कभी बन्धु, कभी साथी, कभी प्रतिस्पर्धी-विरोधी रह चुका हूं। यह जन्म-मरण चक्र अनादि है। आप एक ही भूमिका से आसक्त हो गए हैं। एक क्षणिक लहर को ही आपने समुद्र मान लिया है.....आदि। राजकुमार के उपदेशों और स्पष्ट कथनों से राजा का मोह समाप्त हुआ।
गर्भोपनिषद् में बताया गया है कि गर्भावस्था में जीव के अन्तःकरण में पूर्वजन्मों की स्मृतियां जागृत होती हैं और वह कहता है—‘‘पूर्वयोनि सरस्राणि दृष्ट्रा चैव ततो मया, आहारा विविधा भुक्ता पीता नानाविधाः स्तनाः जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः। यन्मया परिजन्स्यार्थेकृतं कर्म शुभाशुभं ।। एकाकी तेन दह्येऽहं गतास्ते फलभोगिनः ।’’
अर्थात् हजारों बार मेरा जन्म हो चुका है, विविध प्रकार के आहार में खा चुका हूं, हजारों माताओं का दूध पी चुका हूं, बार-बार पैदा हुआ हूं और बार-बार मरा हूं। आत्मीयों के लिए शुभ और अशुभ कर्म किए हैं। पर वे तो आज साथ हैं नहीं। साथ हैं मेरे कर्म ही उनका ही। फल मुझे मिल रहा है।
इस प्रकार वस्तुतः आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मात्र शरीर की होती है और वह अटल-अनिवार्य है। उसके लिए दुःख करना व्यर्थ है। क्योंकि उस शरीर की चमड़ी से तो प्यार-सम्बन्ध था नहीं। यदि होता तो चमड़ी अभी भी सामने है। फिर न तो वह दुःख का कारण बनती नहीं उसे जलाने-दफनाने का प्रयास होता। स्नेह-अनुराग तो उस शरीर के माध्यम से अब तक क्रियाशील चैतन्य आत्मा से था। वह आत्मा नष्ट हुई नहीं है। इसलिए शोक-क्लेश का न तो कोई कारण है न ही औचित्य। शरीर को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता और आत्मा की मृत्यु कभी हो नहीं सकती। तब फिर कष्ट और रुदन की क्या बात है?
आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होता है और उसी के साथ मर जाता है यह मान्यता पिछले दिनों पदार्थ विज्ञानियों की रही है वे प्राणी को एक चलने-फिरने और सोचने-बोलने वाला समर्थ पौधा मानते रहे हैं। पौधे के जन्म और मरण के साथ ही उसके अस्तित्व का उदय और अन्त ज्ञानी और विज्ञानी एक समान मानते हैं।
प्रश्न प्राणियों के विशेषतया मनुष्य के सम्बन्ध में उपस्थित होता है क्योंकि उसके समाधान से हमारा सीधा सम्बन्ध है। क्योंकि तब सोचना पड़ेगा कि यदि जीवन शरीर के बाद भी बना रहता है तो शरीर त्याग के बाद उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग, नरक, परलोक के प्रसंग इसी सन्दर्भ में सामने आते हैं। यदि पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की स्थिति का इस जन्म पर और इस जन्म का अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? इतना ही नहीं इस सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकला हो उससे वर्तमान जीवन का उपयोग करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने की बात भी सामने आ खड़ी होती है।
सामान्यतया हम भूतकाल से बहुत कुछ सीखते हैं। याद रखते हैं और भावना पूर्वक उस सब को स्मरण रखते हैं जो हमने खोया या पाया है। वर्तमान में जो कुछ हम हैं वह भूतकाल में रोपे गये वृक्ष के ही फल-फूल हैं। भविष्य में कुछ बनता है वह आज के क्रिया-कलाप का प्रतिफल ही होगा। इन दिनों में जो कुछ करते हैं उसका लाभ तत्काल तो मिलता नहीं—कुछ समय उपरांत ही उसके परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार हमारी समस्त गतिविधियां प्रायः भविष्य निर्माण में ही नियोजित रहती हैं। फिर यदि जीवन मरने के बाद भी बना रहता है तो स्वभावतः उसकी भी चिन्ता करनी पड़ेगी और भविष्य के लिए सुखद अवसर प्राप्त करने की तैयारी को भी महत्व देना होगा। यदि जीवन शरीर के साथ ही समाप्त होता है तो मरणोत्तर जीवन के बारे में चिन्ता या तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तब वर्तमान शरीर के वर्तमान और भविष्य को ही सब कुछ मानकर तदनुरूप जीवन यापन की नीति निर्धारित करनी होगी। दोनों परिस्थितियों में दृष्टिकोण अपनाने और कार्यक्रम निर्धारित करने में भारी अन्तर होगा। आस्तिकों को मरणोत्तर भविष्य निर्माण करने के लिए स्वर्ग मुक्ति-शान्ति, सद्गति की बात सोचनी पड़ती है और इस जीवन में तप, संयम, दान, परमार्थ जैसे धर्मानुष्ठानों को महत्व देना पड़ता है भले ही प्रत्यक्षतः उसमें आर्थिक हानि एवं शारीरिक असुविधाएं ही सहन क्यों न करनी पड़ती हों। इसके विपरीत नास्तिक तात्कालिक आमोद-प्रमोद एवं सुख-साधनों को ही महत्व देते हैं। जब देह भस्मीभूत ही ठहरा और पुनरागमन की सम्भावना नहीं रही तो ‘ऋणं कृत्वा घतं पिवेत्’ की नीति अपनाने में कोई अनौचित्य नहीं कहा जा सकता। जीवन का आदि अन्त शरीर तक ही सीमित है या उसके पश्चात् भी उसका अस्तित्व है, यह मात्र दार्शनिक पहेली नहीं है। उसका आज की गतिविधियों से सीधा सम्बन्ध है। एक निश्चय के उपरान्त एक दिशा में चलना पड़ता है और दूसरा निश्चय होने पर दूसरी दिशा में चलने की आवश्यकता अनुभव की जायगी।
क्या मृत्यु की अनुभूति कभी हो सकती है? इसका उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है। मैं मरने वाला हूं, मर रहा, जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए भी कहने वाला अपने को जीवित ही अनुभव करता है। सपने में अपनी मृत्यु का दृश्य देखा जा सकता है। शरीर अचेतन पड़ा हुआ और स्वजन सम्बन्धी रोते कलपते दिखाई पड़ते हैं। इतने पर भी अपनी सत्ता बनी ही दिखती है। मरण का अनुभव अपने को ही होता रहता है। इससे स्पष्ट है कि अपना मरण स्वीकार करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है।
जिसका जो स्वभाव है वह उसे पसन्द होता है और उसकी पूर्ति में प्रसन्न होता है। मछली का जल जीवन स्वभाव है, मच्छर गन्दगी पसन्द करते हैं और खटमल रक्त पीते हैं। इसमें उन्हें घृणा नहीं प्रसन्नता होती है। आत्मा यदि मरणधर्मा होता तो उसे मरने से तनिक भी डर न लगता। चूंकि वह मरना नहीं चाहता, मृत्यु संकट आने पर उससे बचने का हर सम्भव उपाय करता है। मरने से डरना यह बताता है कि मृत्यु अस्वाभाविक है। जीवात्मा उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यों शरीर मरता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती तो भी उसे न केवल अपनी वरन् अपने शरीर और स्वजनों तक की मृत्यु अनुपयुक्त अप्रिय लगती है। जीवन ही आत्मा का धर्म है। अपना मरण तो होता नहीं है। शरीरों पर पदार्थों के लिए मरण स्वाभाविक होते हुए भी चेतना पर उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। यह सब लक्षण इस बात के हैं कि मानवी सत्ता मरणशील नहीं न उसे मरण से कोई सहानुभूति है।
स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग अस्वाभाविक। स्वस्थ सदैव बने रहने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं। अस्वस्थता थोड़े दिन की भी असह्य होती है। किसी प्रियजन के रोगी होने से चिन्ता होती है उसकी स्थिति तथा वजह पूछने जानने के लिए आतुरता व्यक्त की जाती है किन्तु स्वस्थ रहने पर कोई उसके लिए चिन्ता नहीं करता और न यह पूछता है कि आप स्वस्थ क्यों हैं? इससे स्वाभाविक और अस्वाभाविक होने का परिचय मिलता है। मृत्यु और जीवन के संबन्ध में भी यही बात है। मृत्यु का समाचार पाकर या उसकी सम्भावना विदित होने पर चिन्ता सम्वेदना प्रकट की जाने लगती है, पर जीवित रहने पर ऐसी कोई व्यग्रता कहीं से भी नहीं होती। इससे जीवन की स्वाभाविकता सिद्ध है। अस्वाभाविक तो मरण ही है। जब शरीर तक के मरण में अस्वाभाविकता मानी जाती है तब आत्मा की चेतन सत्ता का मरण स्वीकार करने की बात तो किसी के गले उतरती ही नहीं।
इस संसार में जितना पदार्थ सृष्टि के आरम्भ में था उतना ही अन्त तक रहेगा। उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। ठोस, तरल और वायु भूत इन स्थितियों में वस्तुयें बदलती रहती हैं। पानी तरल है, ठण्डक पड़ने पर बर्फ बन जाता है। गर्मी पड़ने पर भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है फिर बादल या ओस बनकर तरल रूप में दिखाई पड़ता है। यही अदला-बदली वस्तुओं की उत्पत्ति और मृत्यु के रूप में प्रकट-अप्रकट होती रहती है, वस्तुतः कोई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। इस सिद्धांत को रसायन शास्त्र के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। भौतिक विज्ञान में इसी सिद्धांत को ‘तत्व का अनुत्पत्तित्व’—तत्व का अतिनाशित्व शक्ति का परिवर्तन—नाम से प्रतिपादित किया गया है। अध्यात्म शास्त्र में पदार्थ और प्राणी दोनों पर ही इसी तथ्य का समान रूप से कार्यान्वयन प्रतिपादित किया गया है। गीता कहती है—‘नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः ।’ अर्थात् जो नहीं था वह पैदा नहीं होता और जो है उसका नाश नहीं हो सकता। इस प्रतिपादन में पदार्थ की तरह आत्मा की अमरता भी सन्निहित है।
किसी से पूछा जाय कि आप का अस्तित्व इस समय है या नहीं, वह यही है, में ही उत्तर दें सकता है। यदि यह ‘मैं’ इस समय विद्यमान है तो वह पहले भी था और आगे भी बना ही रहेगा। हां, नाम, रूप और स्थान का परिवर्तन प्रकृति के स्वाभाविक क्रम के अनुसार अवश्य होता रहता है। यदि स्थानान्तरण को मृत्यु समझा जाय तब तो बात दूसरी है पर यदि विनाश या समाप्ति के रूप में मरण की व्याख्या की जाती हो वह भौतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों ही दृष्टियों से गलत है। आत्मा का अस्तित्व शरीर की मृत्यु होने के उपरान्त भी बना रहता है। इस तथ्य से वे धर्म भी इनकार नहीं करते जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। उस परलोक का अस्तित्व तो उन्हें भी मान्य है, जिसमें मरने के बाद भी आत्मा किसी न किसी स्थिति में निवास करता रहता है।
साधारणतया जन्म शब्द का अर्थ पैदा होना और मृत्यु का नष्ट एवं समाप्त हो जाना है। यह दो घटनायें समझी जाती हैं। संस्कृति भाषा में ‘जन्म’ और ‘मृत्यु’ शब्दों की व्याख्या व्युत्पत्ति में तथ्य को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। उसमें जन्म का अर्थ प्रकट होना और मृत्यु का देखने योग्य न रहना भर है। इन शब्दों में स्थिति के परिवर्तन भर का संकेत है किसी नवीन उत्पादन या आत्यंतिक विकास का प्रतिपादन नहीं है।
संस्कृत की ‘जनी-प्रादुभावे’ धातु से जन्म शब्द बना है। प्रादुर्भाव का अर्थ है—प्रकटीकरण-आकिजिन। प्रकट होने का तात्पर्य है जो छिपा था उसका सामने आ जाना ‘जन्म’ शब्द का दूसरा पर्यायवाचक है। उत्पत्ति यह शब्द उद्-पद् से मिलकर बना है। जिनका अर्थ है ऊपर आना। इस व्याख्या में भी स्थिति के बदलने भर का संकेत है। जन्म के पर्याय वाचकों में एक और शब्द है—‘सृष्टि’ क्रिएशन। यह शब्द (सृज-विसर्गे) धातु से बना है। जिसका तात्पर्य भी लगभग वैसा ही है जैसा कि जन्म एवं उत्पत्ति का। सृष्टि को बाहर आना-प्रत्यक्ष होना कह सकते हैं। हमारी इन्द्रियों में सब कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं है। वे पंचतत्वों से बनी होने के कारण मात्र किन्हीं वस्तुओं की स्थूल स्थिति को ही देख सकती है। कितनी ही वस्तुओं का अस्तित्व सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से—रेडियो टेलिस्कोपों से एवं अन्यान्य साधनों से जाना जा सकता है आंखें एवं इन्द्रियां तो वायु भूत पदार्थों तक को नहीं देख पातीं, जबकि अन्य इन्द्रियां उनकी उपस्थिति का अनुभव करती हैं। आग पर मिर्च जला देने से वे हवा में उड़ जाती हैं। तब उस वायु भूत मिर्च को आंखें नहीं देखतीं किन्तु नाक गन्ध रूप में उसकी उपस्थिति अनुभव करती है। इसके आगे सूक्ष्मता आने पर वे इन्द्रियों की पकड़ से बाहर हो जाती है तो भी उनका अप्रकट अस्तित्व बना रहता है। पदार्थ और आत्मा दोनों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त एक समान लागू होता है। जन्म का अर्थ नवीन उत्पत्ति नहीं किन्तु अप्रकट का प्रकट भर हो जाना है।
‘मृत्यु’ शब्द का संस्कृत भाषा में जो अर्थ है उससे भी वस्तुस्थिति पर भली प्रकार प्रकाश पड़ता है। मृत्यु के लिए नाश शब्द का प्रयोग होता है। ‘नाश-नश-अदर्शने’ धातु से बना है। जिसका तात्पर्य है—देखने योग्य न रहना। इसमें अस्तित्व के अभाव की बात नहीं कही गई है, मात्र इतना ही संकेत है कि वह पदार्थ दृष्टि पथ से ओझल हो गया। ऐसा तो बच्चे ‘आंख मिचौनी’ खेल में भी करते रहते हैं। बादलों की छाया सूर्य चन्द्र तक को गुप्त प्रकट होने तक के लिए विवश करती रहती है। धूप-छांव की स्थिति को सूर्य चन्द्र की उत्पत्ति या समाप्त तो नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार आत्मा के शरीर धारण करने और चोला उतार देने की स्थिति के सम्बन्ध में समझा जाना चाहिए। इसमें अस्तित्व तो बना ही रहता है। उसकी अमरता में कोई अन्तर नहीं आता।
मौत से न डरने की जरूरत है और न उसके लिए उतावले होने की। शरीर ही बदलते हैं आत्मा के अस्तित्व पर मौत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कपड़े बार-बार बदलने पड़ते हैं पर शरीर वही बना रहता है—शरीर भी कपड़े की तरह बदलते रहते हैं। जीवन ईश्वर के समान ही अनादि और अनन्त है। कोई सत्कर्म किया है तो उसका फल अगले दिन—अगले जनम में मिल सकता है उसमें अधीरता की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध हो गये मरने के दिन आ गये। अब पढ़ कर क्या करेंगे? अब के आरम्भों का अपने को क्या प्रतिफल मिलेगा, इस तरह नहीं सोचा जाना चाहिए। जीवन अनन्त है। भविष्य सुविस्तृत है। रात्रि में विश्राम करना पड़ता है और काम में व्यवधान पड़ता है यह सोचकर बहुत दिन में पूरी होने वाली योजना बनाने में कोई संकोच नहीं करता। फिर हमीं अनन्त जीवन में क्रमिक गति से आत्मोत्कर्ष की—सद्गुणों की—सद्ज्ञान की सम्पदा एकत्रित करने में कटिबद्ध क्यों न रहें?
इन मान्यताओं को अपनाये रहकर हम शरीर की मृत्यु निश्चित मानते हुए भी अजर-अमरों जैसा निश्चिन्त प्रसन्न और योजनाबद्ध प्रगतिशील जीवन जी सकते हैं। साथ ही आत्मीयों की मृत्यु को मात्र शरीर-परिवर्तन समझकर उसके लिए विलाप करने से बचे रह सकते हैं। इससे दिवंगत आत्मीय भी क्षुब्ध-दुःखी होने से बचेंगे। हमारा दिन नहीं शुभचिन्तन ही उन्हें तृप्ति सन्तोष और शक्ति देगा।
मृत्यु जीवन का अन्त नहीं
महान् धर्मात्मा राजा जनश्रुति को जब भोग-विलास से वैराग्य हुआ तो उसने देखा कि अब तो उसका शरीर भी जर्जर हो चुका है। शरीर में तप और साधना की शक्ति भी नहीं रही। जीवन भर अज्ञान में अनेक पाप किये उनका पश्चात्ताप राजा को दलने लगा तो वह महामुनि रैक्य के पास पहुंचे और बोले भगवन् मैं धर्म चित्त हुआ राजा आज जीव भाव से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मुझे बतलाइये मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या मेरी असहाय चेतना भी जन्म मृत्यु के बन्धन से मुक्ति पा सकती है। महामुनि रैक्य ने बताया—राजन्! जब मृत्यु का समय आता है तब सब इन्द्रियों की वृत्ति वाणी में लय हो जाती है। वाणी की वृत्ति मन में और मन की वृत्ति तब प्राण में परिवर्तित हो जाती है। जागृत अवस्था में पांच कर्मेन्द्रियां और पांच ज्ञानेन्द्रियां मन की इच्छाओं पर नाचती थीं पर मृत्यु के समय मन प्राण चेतना के वश में चला जाता है तब प्राण ही जीवन भर की स्थिति के अनुरूप नये निर्माण में जुट जाते हैं वह निर्माण चाहे अच्छा हो या बुरा उसका निर्णय चेतना के शरीर छोड़ते समय ही हो जाता है। जो लोग ईश्वर उपासना, तप, ज्ञान सम्वर्धन और साधना द्वारा अपना मनोबल और आत्म-बल विकसित कर लेते हैं वह अनेक गुणों और संस्कारों से युक्त सुन्दर जीवन पाते हैं और जिनकी इन्द्रियों के प्रति लालसा जागृत बनी रहती है वे उन-उन इच्छाओं की पूर्ति के लिये पुनः कोई शरीर धारण करते हैं। यह पटाक्षेप सनातन काल तक चलते रहते हैं।
उपरोक्त कथन में मृत्यु विज्ञान पर जहां संक्षिप्त शास्त्रीय प्रकाश डाला गया है वहां यह समझाने का प्रयत्न भी है कि एक मृत्यु के बाद मनुष्य का अन्त नहीं हो जाता वरन् उसे अपने कर्मानुसार अन्य जन्म भी धारण करने पड़ते हैं। बार-बार जन्म और बार-बार मृत्यु होती है। जब तक सृष्टि का प्रत्येक जीव पूर्णता नहीं प्राप्त कर लेता यह प्रक्रिया कभी बन्द न होगी।
एक बार बालक नचिकेता को भी ऐसी ही प्रबल जिज्ञासा उठी थी, उसने भी यमाचार्य से ऐसा ही प्रश्न किया था—
ये यंप्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्ये के नत्यमस्तीति चान्ये । एतद्विद्यामनुशिष्ट सत्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ।। —कठ. उप. 1-20
‘‘आचार्यदेव! मरे हुये मनुष्य के विषय में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं, मृत्यु हो जाने पर भी जीव बना रहता है। कुछ कहते हैं, उसका नाश हो जाता है। सो आप मुझे उसका निश्चित निर्णय करके बताइये सत्य क्या है?’’
यमाचार्य ने नचिकेता को तब योगाभ्यास कराया और उसके द्वारा उसने यह जाना कि जीव किस प्रकार मृत्यु के उपरान्त यमलोक, प्रेतलोक, वृक्ष, वनस्पति आदि योनियों, भुवर्लोक आदि में जाता है और वहां की परिस्थितियों का वर्तमान जीवन की तरह उपयोग करता है।
Write Your Comments Here:
- धीरे-धीरे आती जाती मृत्यु समीप
- मृत्यु की मीठी गहरी नींद जरूरी
- अर्धमृत न रहें, पूर्ण जीवित बनें
- मरण सृजन का अभिनव पर्व—उल्लासप्रद उत्सव
- आसक्ति मनुष्य को मृत्यु के बाद भी घुमाती है
- मृतात्मा को क्षुब्ध नहीं, तृप्त करें
- सुदीर्घ विश्राम की अवधि को सार्थक बनाएं
- पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को क्रिया से जोड़ें