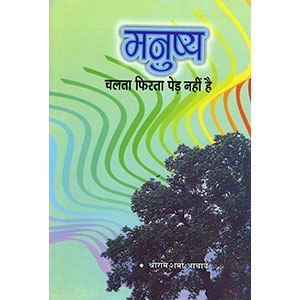मनुष्य चलता फिरता पेड़ नही है 
आत्मा का अस्तित्व—एक गम्भीर प्रश्न
Read Scan Version
एक प्रश्न जो सदियों से अब तक उलझता हुआ आ रहा है वह है—आया - शरीर से प्रथक - आत्मा - नाम की कोई सत्ता वस्तुतः है अथवा नहीं। भौतिकतावादी दृष्टिकोण ने प्रत्यक्ष को प्रमाण के आधार पर इस मान्यता से इनकार किया है कि चेतना कोई ऐसा तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी बना रहता है और अनेक योनियों में विचरण करता हुआ अपनी सनातन जीवन यात्रा पूर्ण करता रहता है। दूसरी ओर साधकों संतों तपस्वी और योगियों ने अपनी अन्तरंग अनुभूतियों के आधार पर आत्म-तत्व का प्रतिपादन किया है और उसे जीवन सत् कह कर उसे देखने सुनने और प्राप्त करने को ही परमार्थ, जीवन लक्ष्य और परम पुरुषार्थ कहा है। प्रत्यक्ष का विराम होने के कारण और नये का उदय होते रहने के कारण प्रत्यक्षवादी बुद्धि भी भ्रमित होती है और अदृश्य को देख न पाने अथवा उसको प्राप्त करने के पीछे आधार भूत तपश्चर्या को पूर्ण न कर सकने के कारण आस्थावादी बुद्धि भी चकराती है यही कारण है कि यह प्रश्न अनादि काल से उलझता सुलझता चला आ रहा है प्रश्न इतना मार्मिक और महत्वपूर्ण है कि उसे निरुत्तरित छोड़ा जाना भी मानव जीवन के हित में नहीं विशेषकर उस स्थिति में जब कि उसके आधार पर जीवन दर्शन निर्धारित होते हैं और उसके भले बुरे परिणाम भी संसार को भुगतने पड़ते हैं।
यह युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने अदृश्य, अप्रकट को स्पष्ट करने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है सच पूछा जाये तो उसने भारतीय दर्शन के आत्मावादी सिद्धान्त को पूरी तरह पुष्ट भी कर दिया है किन्तु प्रायः विज्ञान जिन के पास है उन्हें आध्यात्म दर्शन के सामीप्य का अवसर नहीं मिला अतएव सूक्ष्म का तथ्यान्वेष कर लेने के बावजूद वैज्ञानिकों के सम्मुख भी यह प्रश्न उलझा का उलझा रहा गया। इसे इस युग की एक अद्भुत उपलब्धि कहा जाना चाहिए कि मानवीय अन्तःकरण ने विज्ञान की संगति आध्यात्म से मिलाकर इस महत्व पूर्ण प्रश्न को सुलझाने का यत्न किया।
मैं और मेरे में उलझी सचाई
मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? इन छोटे से प्रश्न का सही समाधान न कर सकने के कारण ‘मैं’ को कितनी कितनी विषम विडम्बनाओं में उलझना पड़ता है और विभीषिकाओं में संत्रस्त होना पड़ता है, यदि यह समय रहते समझा जा सके तो हम वह न रहें, जो आज है। वह न सोचें जो आज सोचते हैं वह न करें जो आज करते हैं। हम कितने बुद्धिमान हैं कि धरती आकाश का चप्पा-चप्पा छान डाला और प्रकृति के रहस्यों को प्रत्यक्ष करके सामने रख दिया। इस बुद्धिमत्ता की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम और अपने आपके बारे में जितनी उपेक्षा बरती गई उसकी उतनी निन्दा की जाय वह भी कम ही है।
जिस काया को शरीर समझा जाता है क्या यही मैं हूं? क्या कष्ट, चोट, भूख, शीत, आतप आदि से पग-पग पर व्याकुल होने वाला अपनी सहायता के लिए बजाज, दर्जी, किसान, रसोइया, चर्मकार, चिकित्सक आदि पर निर्भर रहने वाला ही मैं हूं? दूसरों की सहायता के बिना जिसके लिए जीवन धारण कर सकना कठिन हो—जिसकी सारी हंसी-खुशी और प्रगति दूसरों की कृपा पर निर्भर हो, क्या वही असहाय, असमर्थ, मैं हूं? मेरी आत्मा निर्भरता क्या कुछ भी नहीं है? यदि शरीर ही मैं हूं तो निस्सन्देह अपने को सर्वथा पराश्रित और दीन दुर्बल ही माना जाना चाहिए।
परसों पैदा हुआ, खेल कूद, पढ़ने-लिखने में बचपन चला गया। कल जवानी आई थी। नशीले उन्माद की तरह आंखों में, दिमाग में छाई रही। चंचलता ओर अतृप्ति से बेचैन बनाये रही। आज ढलती उम्र आ गई। शरीर ढलने गलने लगा। इन्द्रियां जवाब देने लगीं। सत्ता बेटे, पोतों के हाथ चली गई। लगता है एक उपेक्षित और निरर्थक जैसी अपनी स्थिति है। अगली कल यही काया जरा जीर्ण होने वाली है। आंखों में मोतियाबिन्द, कमर घुटनों में दर्द खांसी, अनिद्रा जैसी व्याधियां, घायल गधे पर उड़ने वाले कौए की तरह आक्रमण की तैयारी कर रही हैं। अपाहिज और अपंग की तरह कटने वाली जिंदगी कितनी भारी पड़ेगी। यह सोचने को जी नहीं चाहता वह डरावना और घिनौना दृश्य एक क्षण के लिए भी आंखों के सामने आ खड़ा होता है तो रोम-रोम कांपने लगता है? पर उस अवश्यंभावी भवितव्यता से बचा जाना सम्भव नहीं? जीवित रहना है तो इसी दुर्दशा ग्रस्त स्थिति में पिसना पड़ेगा। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। क्या यही मैं हूं? क्या इसी निरर्थक विडम्बना के कोल्हू के चक्कर काटने के लिए ही ‘मैं’ जन्मा? क्या जीवन का यही स्वरूप है? मेरा अस्तित्व क्या इतना ही तुच्छ है।
आत्म चिन्तन कहेगा—नहीं-नहीं-नहीं। आत्मा इतना हेय और हीन नहीं हो सकता। वह इतना अपंग और असमर्थ-पराश्रित और दुर्बल कैसे होगा? यह तो प्रकृति के पराधीन पेड़-पौधों जैसा—मक्खी, मच्छरों जैसा जीवन हुआ। क्या इसी को लेकर-मात्र जीने के लिए मैं जन्मा। सो भी जीना ऐसा जिसमें न चैन, न खुशी, न शान्ति, न आनन्द, न सन्तोष। यदि आत्मा—सचमुच परमात्मा का अंश है तो वह ऐसी हेय स्थिति में पड़ा रहने वाला हो ही नहीं सकता। या तो मैं हूं ही नहीं। नास्तिकों के प्रतिपादन के अनुसार या तो पांच तत्वों के प्रवाह में एक भंवर बबूले जैसी क्षणिक काया लेकर उपज पड़ा हूं और अगले ही क्षण अभाव के विस्मृति गर्त में समा जाने वाला हूं। या फिर कुछ हूं तो इतना तुच्छ और अपंग हूं जिसमें उल्लास और सन्तोष जैसा—गर्व और गौरव जैसा—कोई तत्व नहीं है। यदि मैं शरीर हूं तो—हेय हूं। अपनी लिए और इस धरती के लिए भारभूत हूं। पवित्र अन्न को खाकर घृणित मल में परिवर्तन करते रहने वाले—कोटि-कोटि छिद्रों वाले इस कलेवर से दुर्गन्ध और मलीनता निसृत करते रहने वाला—अस्पर्श्य—घिनौना हूं ‘मैं’। यदि शरीर हूं तो इससे अधिक मेरी सत्ता होगी भी क्या?
मैं यदि शरीर हूं तो उनका अन्त क्या है? लक्ष्य क्या है? परिणाम क्या है?—मृत्यु—मृत्यु—मृत्यु। कल नहीं तो परसों वह दिन तेजी से आंधी तूफान की तरह उड़ता उमड़ता चला आ रहा है, जिसमें आज की मेरी यह सुन्दर सी काया—जिसे मैंने अत्यधिक प्यार किया—प्यार क्या जिसमें पूरी तरह समर्पित हो गया—धुल गया। अब वह मुझसे विलग हो जायगी। विलग ही नहीं अस्तित्व भी गंवा बैठेगी। काया में घुला हुआ ‘मैं’—मौत के एक ही थपेड़े में कितना कुरूप—कितना विकृत—कितना निरर्थक—कितना घृणित हो जायगा कि उसे प्रिय परिजन तक—कुछ समय और उसी घर में रहने देने के लिए सहमत न होंगे जिसे मैंने ही कितने अरमानों के साथ—कितने कष्ट सह कर बनाया था। क्या यही मेरे परिजन हैं? जिन्हें लाड़ चाव से पाला था। अब ये मेरी इस काया को—घर में से हटा देने के लिए—उसका अस्तित्व सदा के लिए मिटा देने के लिए क्यों आतुर हैं? कल वाला ही तो मैं हूं।
मौत के जरा से आघात से मेरा स्वरूप यह कैसा हो गया। अब तो मेरी मृत काया—हिलती डुलती भी नहीं—बोलती, सोचती भी नहीं? अब तो उसके कुछ अरमान भी नहीं हैं। हाय, यह कैसी मलीन दयनीय, घिनौनी बनी जमीन पर लुढ़क रही है। अब तो यह पलंग बिस्तर पर सोने तक का अधिकार खो बैठी। कुशाओं बान से ढकी—गोबर से लिपी गीली भूमि पर यही पड़ी है। अब कोई चिकित्सक भी इसका इलाज करने को तैयार नहीं। कोई बेटा, पोता गोदी में नहीं आता। पत्नी छाती तो कूटती है पर साथ सोने से डरती है। मेरा पैसा—मेरा वैभव—मेरा सम्मान हाय रे सब छिन गया—हाय रे मैं बुरी तरह लुट गया। मेरे कहलाने वाले लोग ही—मेरा सब कुछ छीन कर मुझे इस दुर्गति के साथ घर से निकाल रहे हैं। क्या यही अपनी दुर्दशा कराने के लिए मैं जन्मा? यही है क्या मेरा अन्त—यही था क्या मेरा लक्ष्य, यही है क्या मेरी उपलब्धि। जिसके लिए कितने अरमान संजोये थे, जिसके लिए कितने पुरुषार्थ किये थे—क्या उसका निष्कर्ष यही हूं? यही हूं मैं—जो मुर्दा बना पड़ा हूं और लकड़ियों की चिता में जल कर अगले ही क्षण अपना अस्तित्व सदा के लिए खोने जा रहा हूं।
लो अब पहुंच गया मैं चिता पर। लो, मेरा कोमल मखमल जैसा शरीर—जिसे सुन्दर, सुसज्जित, सुगन्धित बनाने के लिए घण्टों श्रृंगार किया करता था, अब आ गया अपनी असली जगह पर। लकड़ियों का ढेर—उसके बीच दबाया दबोचा हुआ मैं!लो यह लगी आग। लो, अब मैं जला। अरे मुझे जलाओ मत। इन खूबसूरत हड्डियों में मैं अभी और रहना चाहता हूं, मेरे अरमान बहुत हैं, इच्छायें तो हजार में से एक भी पूरी नहीं हुई। मुझे मरी उपार्जित सम्पदाओं से अलग मत करो, प्रियजनों का वियोग मुझे सहन नहीं। इस काया को जरा सा कष्ट होता था तो चिकित्सा, उपचार मैं बहुत कुछ करता था। इस काया को इस निर्दयता पूर्वक मत जलाओ। अरे स्वजन और मित्र कहलाने वाले लोगों—इस अत्याचार से मुझे बचाओ। अपनी आंखों के आगे ही मुझे इस तरह जलाया जाना तुम देखते रहोगे। मेरी कुछ भी सहायता न करोगे अरे यह क्या—बचाना तो दूर उलटे तुम्हीं मुझ में आग लगा रहे हो। नहीं—नहीं मुझे जलाओ मत—मुझे मिटाओ मत। कल तक मैं तुम्हारा था—तुम मेरे थे—आज ही क्या हो गया जो तुम सबने इस तरह मुझे त्याग दिया? इतने निष्ठुर तुम सब क्यों बन गये? मैं और मेरा संसार क्या इस चिता की आग में ही समाप्त हुआ? सपनों का अन्त—अरमानों का विनाश—हाय री चिता—हत्यारी चिता, तू मुझे छोड़। मरने का जलने का मेरा जरा भी जी नहीं है। अग्नि देवता, तुम तो दयालु थे। सारी निर्दयता मेरे ही ऊपर उड़ेलने के लिए क्यों तुल गये?
लो, सचमुच मर गया। मेरा काया का अन्त हो ही गया। स्मृतियां भी धुंधली हो चलीं। कुछ दिन चित्र फोटो जिसे। श्राद्ध तर्पण का सिलसिला कुछ दिन चला। दो तीन पीढ़ी तक बेटे पोतों का नाम याद रहे। पचास वर्ष भी पूरे न हो पाये कि सब जगह से नाम निशान मिट गया। अब किसी को बहुत कहा जाय कि इस दुनिया में ‘मैं’ पैदा हुआ था। बड़े अरमानों के साथ जिया था जीवन को बहुत संजोया, संभाला था, उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर वह सारी दौड़, धूप ऐसे ही निरर्थक चली गई। मेरा काया तक ने मेरा साथ न दिया—जिसमें मैं पूरी तरह घुल गया था। जिस काया के सुख को अपना सुख और जिसके दुख को अपना दुख समझा। सच तो यह है कि मैं ही काया था—और काया ही मैं था हम दोनों की हस्ती एक हो गई थी, पर यह क्या अचंभा हुआ, मैं अभी मौजूद हूं।
वायुभूत हुआ आकाश में मैं अभी भी भ्रमण कर रहा हूं। पर वह मेरी अभिन्न सहचरी लगने वाली काया न जाने कहां चली गई। अब वह मुझे कभी नहीं मिलेगी क्या? उसके बिना मैं रहना नहीं चाहता था रह नहीं सकता था, पर हायरी निर्दय नियति। तू ने यह क्या कर डाला। काया चली गई। माया चली गई। मैं अकेला ही वायु भूत बना भ्रमण कर रहा हूं। एकाकी-नितान्त एकाकी। जब काया ने ही साथ छोड़ दिया तो उसके साथ जुड़े हुए परिवारी भी क्या याद रखते—क्यों याद रखते? याद रखे भी रहे हों तो अब उससे अपना बनना भी क्या है?
मैं काया हूं। यह जन्म के दिन से लेकर—मौत के दिन तक मैं मानता रहा। यह मान्यता इतनी प्रगाढ़ थी कि कथा पुराणों की चर्चा में आत्मा काया की प्रथकता की चर्चा आये दिन सुनते रहने पर भी गले से नीचे नहीं उतरती थी। शरीर हो तो मैं हूं—उससे अलग मेरी सत्ता भला किस प्रकार हो सकती है? शरीर के सुख-दुख के अतिरिक्त मेरा सुख-दुख अलग क्योंकर होगा? शरीर के लाभ में अन्तर कैसे माना जाय? यह बातें न तो समझ में आती थीं ओर न उन पर विश्वास जमता था। परोक्ष पर प्रत्यक्ष कैसे झुठलाया जाय? काया प्रत्यक्ष है—आत्मा अलग है, उसके स्वार्थ, सुख दुख अलग हैं, यह बातें कहने सुनने भर की ही हो सकती हैं। सो रामायण गीता वाले प्रवचनों की हां में हां तो मिलाता रहा पर उसे वास्तविकता के रूप में कभी स्वीकार न किया।
पर आज देखता हूं कि वह सचाई थी जो समझ में नहीं आई और वह झुठाई थी जो सिर पर हर घड़ी सवार रही। शरीर ही मैं हूं। यही मान्यता—शराब की खुमारी की तरह नस-नस में भरी रही। बोतल छानता रहा तो वह खुमारी उतरती भी कैसे? पर आज आकाश में उड़ता हुआ वायुभूत—एकाकी—‘मैं’ सोचता हूं। झूठा जीवन जिया गया। झूठ के लिए जिया गया, झूठे बनकर जिया गया। सचाई आंखों से ओझल ही बनी रही। मैं एकाकी हूं, शरीर से भिन्न हूं। आत्मा हूं। यह सुनता जरूर रहा पर मानने का अवसर ही नहीं आया। यदि उस तथ्य को जाना ही माना भी होता तो वह अलभ्य अवसर जो हाथ से चला गया, इस बुरी तरह न जाता। जीवन जिस मूर्खतापूर्ण रीति-नीति से जिया वैसा न जिया जाता।
शरीर मेरा है—मेरे लिए है, मैं शरीर नहीं हूं। यह छोटी सी सचाई यदि समय रहते समझ में आ गई होती तो कितना अच्छा होता। तब मनुष्य जीवन जैसे सुरदुर्लभ सौभाग्य का लाभ लिया गया होता, पर अब क्या हो सकता है। अब तो पश्चात्ताप ही शेष है। भूल भरी मूर्खता के लिए न जाने कितने लम्बे समय तक रुदन करना पड़ेगा?
शरीर ही नहीं आत्मा को भी देखें
शरीर और आत्मा की प्रथकता को जानते बहुत हैं, पर मानते कोई-कोई ही हैं। मरने के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है, इसे प्रत्येक धर्मावलम्बी मानता है। हिन्दू—धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता को पूरी तरह स्वीकार किया गया है। ईसाई, मुसलमान पुनर्जन्म तो नहीं मानते पर मरणोत्तर जीवन स्वीकार करते हैं। शरीर न रहने पर भी आत्माओं का बना रहना और ब्रह्म-लोक में प्रलय के दिन उनके क्रियाकलाप को उचित-अनुचित ठहराया जाना उनके यहां भी स्वीकारा गया है। इन सभी स्थितियों में मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहने की बात को माना गया है।
अतीन्द्रिय विज्ञान भी क्रमशः इसी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है कि कुछ समय पूर्व भौतिक—विज्ञानवेत्ता शरीर से प्रथक कोई स्वतन्त्र आत्मा न होने की जिस बात को जोरों के साथ कहते हैं, अब वह बात कुछ दमदार नहीं रही। पूर्वजन्मों की स्मृतियों वाले बालक उन ईसाई और मुसलमान—परिवारों में भी पाये गये हैं, जिनकी परम्परा पूर्वजन्म स्वीकार न करने की ही रही है। कितने ही बालक संगीत आदि की ऐसी अद्भुत प्रतिभा अतिन्यून आयु में ही प्रदर्शित करते हैं, जिसका मानव मस्तिष्क-विकास के स्वाभाविक—विकास के साथ कोई ताल-मेल नहीं खाता। इन अद्भुत उदाहरणों का समाधान ‘‘पूर्व जन्मों की विद्या का अनायास प्रकटीकरण’’ मानने के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं होता।
भूत-प्रेतों के अस्तित्व को विज्ञ-समाज में अन्ध विश्वास और वहम भर माना जाता रहा है। पर कठोर अन्वेषण की परीक्षा—कसौटी पर खरे उतरने वाले प्रमाण सामने आये हैं, जिनमें भूतात्माओं के अस्तित्व से इन्कार करने की गुंजाइश नहीं रहती। प्रचलित भूतवाद के ढकोसलों में बहुत कुछ ‘वहम’ हो सकता है, पर यत्र-तत्र ऐसे भी प्रमाण सामने आते हैं—जिन्हें देखते हुए मरण के उपरान्त भी आत्माओं के किसी रूप में बने रहने और हलचलें करने की बात को स्वीकार करना ही पड़ता है।
नव-जात शिशुओं में माता का दूध पीने का स्थान ढूंढ़ निकालना आदि कितनी ही ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिन्हें देखते हुए यही मानना पड़ता है कि पूर्वसंचित ज्ञान के बिना यह सब अनायास ही नहीं हो सकता। अनुवांशिकी-विज्ञान में पैतृक ज्ञान के फलित होने का प्रतिपादन अवश्य है, पर वह भी यहां आश्चर्य चकित है कि बिना प्रशिक्षण या बिना आधार के जीव धारियों के बालक कैसे जीवनोपयोगी रीति-नीति ही विकसित कर लेते हैं? पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते रहने वाले पक्षी किस प्रकार मार्ग की दुर्लभ्य कठिनाइयों को नपे-तुले ढंग से पार करते हैं और कुछ विशेष प्रकार की ईल जैसी मछलियां कैसे सहस्रों मील की यात्रा करने प्रणय-प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान पर जाती और फिर वर्षों में पूरी होने वाली उस लम्बी यात्रा को पूरी करके यथा स्थान वापिस लौटती हैं? प्राणियों के सहज ज्ञान की श्रृंखला इतनी विलक्षण है कि वंशानुक्रम की सम्भावनाएं उसका समाधान कर नहीं पातीं। कीव-विज्ञानी अब यह सोचने लगे हैं कि इस संचित ज्ञान का आधार जीवधारियों के पुनर्जन्म से सम्बन्धित होना चाहिए।
जो हो, किसी न किसी आधार पर प्रायः हर वर्ग का व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मृत्यु के बाद ही जीवन का अन्त नहीं हो जाता, वरन् पीछे भी बना रहता है। शरीर के बिना भी जो जीवित रहता है, उसे आत्मा ही कहा जायगा। इस प्रकार यह मरणोत्तर जीवन की मान्यता आस्तिकों तक ही सीमित नहीं रही, वरन् नास्तिक वर्ग भौतिक प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य को क्रमशः स्वीकार करता चला जा रहा है।
प्रश्न यह है कि जब शरीर से प्रथम आत्मा के अस्तित्व की जानकारी प्रायः सभी को है और हलके-भारी मन से उस तथ्य को किसी न किसी रूप में स्वीकार हो जाना है तो हमारा यह प्रयास क्यों नहीं होता कि आत्मा के ऐसे स्वार्थों की ओर भी ध्यान दिया जाय, तो शरीर से ही जुड़े हुए नहीं हो सकते। शरीर-सुख में इन्द्रिय-जन्य वासनाओं की तृप्ति ही मुख्य है। मन की मांग अदंता के पोषण करने वाली वस्तुओं तथा परिस्थितियों को जुटाने की रहती है। मोटे रूप से वासना और तृष्णा ही शरीर-सुख के दो आधार पाये जाते हैं। किन्तु देखा जाता है कि जिनके पास यह साधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं उनका भी अन्तःकरण इन उपलब्धियों से सन्तुष्ट नहीं होता, वरन् बहुत कुछ मिलने पर भी अशान्त, अतृप्त और उद्विग्न ही बना रहता है। अन्तरंग के मर्मस्थल में यह असन्तुष्ट सत्ता कौन है? निस्सन्देह इसे आत्मा ही कहा जायगा।
शरीर की मांग—भूख, वासना और तृष्णा के साधन जुटने पर तृप्त होनी चाहिए। होती भी है। भरपेट स्वादिष्ट आहार मिल जाने पर फिर उसकी अधिक मात्रा खाते नहीं बनती। काम-सेवन आदि की भी एक स्वल्प सीमा है। तृप्ति के बाद उस सन्दर्भ में भी जी ऊब जाता है, यही बात अन्य सब इन्द्रियों के बारे में भी है। तृप्ति के साधन जुट जाने के बाद भी जो घोर अतृप्त पाया जाता है, वह अन्तरात्मा ही है। उसकी आकांक्षाएं शरीर से भिन्न हैं। जब तक उन्हें पूरा करने के साधन न जुटें, तब तक उसका असन्तुष्ट रहना स्वाभाविक भी है। शरीर और आत्मा की भिन्नता और उनके पारस्परिक सम्बन्धों, स्वार्थों को समझने का नाम ही अध्यात्म है। जब तक वह भिन्नता समझी-स्वीकारी न जाय, तब तक मात्र शरीर का पोषण करने वाले प्रयास ही होते रहते हैं। आत्मा की स्थिति और आवश्यक समझे बिना उसके लिए कुछ सोचा किया भी कैसे जाय? इस एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह ही कहना चाहिए कि हम अपने आपको भूल बैठे हैं। अपने आपको अर्थात् आत्मा को। शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा अप्रत्यक्ष। चमड़े से बनी आंखें और मज्जा-तन्तुओं से बना मस्तिष्क केवल अपने स्तर के शरीर और मन को ही देख-समझ पाता है। जब तक चेतना-स्तर इतने तक ही सीमित रहेगा, तब तक शरीर और मन की सुख सुविधाओं की बात ही सोची जाती रहेगी। उससे आगे बढ़कर इस तथ्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकना सम्भव ही न होगा कि हमारी—आत्मा का—स्वरूप एवं लक्ष्य क्या है और आन्तरिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जा सकता है?
चिरस्थायी और गहन अन्तराल की तृप्ति को शान्ति कहते हैं और शरीर, मन की आकांक्षा पूर्ति कहलाती है। लोग सुख के लिए उछल-कूद करते रहते हैं, किन्तु शान्ति के सम्बन्ध में सोचते भी नहीं। फिर वह मिले कैसे? अशान्त अन्तःकरण की जलन-सुख साधनों की कुछ बूंदों से शान्त नहीं हो सकती। यही कारण है की धनाधीश, सत्ताधारी और सम्मानित व्यक्ति आन्तरिक दृष्टि से विक्षुब्ध ही बने रहते हैं। सूक्ष्म तत्वों को देखने—समझने के लिए एक विशेष दिव्य—दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, अध्यात्म की भाषा में उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। गायत्री—मन्त्र में इसी दिव्य प्रकाश को सविता का भर्ग मानकर उपास्य ठहराया गया है। यह दिव्य-दृष्टि जगे तो शरीर और मन्त्र के घेरे से ऊंचे उठकर वस्तु स्थिति को देखना—समझना सम्भव हो सकता है।
मोटी दृष्टि हमें शरीर और मन की परिधि तक ही सीमित रखती है। स्थूल पदार्थों के चिन्तन तक ही उसकी पहुंच है। आत्म-कल्याण की बात उस दृष्टि से सोची जाय तो पंच-तत्वों से बने धर्मोपकरणों का, तीर्थ—मन्दिर दान, उपवास जैसे साधनों का ही उपयोग करने की ही बात सूझती है।
आत्म-शान्ति का स्वरूप क्या हो सकता है? उसकी कल्पना स्वर्ग में आहार निवास उपभोग के प्रचुर साधनों की परिधि तक ही कल्पना करती है। मानो मरने के उपरान्त भी आत्मा वर्तमान शरीर को ही धारण किये रहेगी और उन्हीं प्रसाधनों के उपभोग से काम चलेगा। यह बात सूझती ही नहीं कि जब वासना-तृष्णा की साधन-सामग्री इस लोक में तृप्ति न दे सकी तो तथाकथित स्वर्ग में बताई गई सुख-सामग्री से आत्मा का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? इस चिन्तन को बचपन ही कहना चाहिए कि आत्म-शान्ति की आन्तरिक तृप्ति के सन्दर्भ में भी वासना-तृष्णा के साधना जुटाने वाले तथाकथित स्वर्गीय परिस्थितियों में ही आनन्द और सन्तोष मिलने की बात सोचें।
आत्मा एक दिव्य चेतना स्फुलिंग है—जिसे भावनात्मक उल्लास से साधनों में ही तृप्ति मिल सकती है। सद्भावनाओं से प्रेरित सत्प्रवृत्तियों में ही आत्मा की शान्ति का उद्गम केन्द्र है। उत्कृष्ट स्तर का चिन्तन जब कार्यरूप में परिणित होता है। तब वह परिस्थिति बनती है, जिसमें आत्मा को शान्ति एवं तृप्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार के आनन्द की आरम्भिक झांकी स्वाध्याय और सत्संग में मिल सकती है, जो काय-कलेवर और आत्मा की मित्रता का—उनके पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन विश्लेषण कर सके एवं वासना-तृष्णा की सुख-लिप्सा से ऊंचे उठकर उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता अपना-कर आन्तरिक उल्लास की उपलब्धि का मार्ग-दर्शन कर सके। विषय-चर्चा से जिस प्रकार कानों को रस मिलता है, मनोरम दृश्य देखकर आंखें जिस प्रकार मुदित होती है, उसी प्रकार आत्म-चेतना को उस उद्बोधन में प्रसन्नता मिलती है, जिसके आधार पर अन्तःकरण को सद्भावनाओं से ओत-प्रोत बनाया जा सके। आत्म-शान्ति का द्वार तब खुलता है, जब सत्प्रवृत्तियों से भरी-पूरी गतिविधियां अपना कर यह अनुभव किया जाता है कि जीवन के स्वरूप और लक्ष्य के अनुरूप गतिविधियां अपना कर अपूर्णता से पूर्णता की ओर कदम बढ़ते चल रहे हैं। उच्च भावनाओं के अनुरूप क्रियाकलाप जब बन पड़ता है तो जीवन-क्रम का वह स्वरूप बन जाता है, जिसमें आत्मा को शान्ति और तृप्ति प्राप्त हो सके, वह भव-बन्धनों से मुक्त होकर नर से नारायण बन सके। शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानना उत्तम है, पर पर्याप्त नहीं। उस ज्ञान का लाभ तब है, जब काय-कलेवर के उचित, आवश्यक स्वार्थों तक ही सीमित रहा जाय और अपनी शेष शक्ति को आत्मिक—शान्ति की, आत्मिक—तृप्ति की, आत्मिक-प्रगति की दिशा में नियोजित किया जाय। कहना न होगा कि यह प्रयोजन उत्कृष्ट—चिन्तन ओर आदर्श कर्तृत्व अपनाने से ही पूरा हो सकता है। जब आत्मा और शरीर की भिन्नता को—उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को समझ ही नहीं लिया जाता, वरन् शरीर की तुलना में आत्मा के महत्व को स्वीकार करते हुए आत्म-कल्याण के प्रयास में तत्पर हुआ जाता है, तब यह माना जाता है कि आत्म-ज्ञान की दिव्य किरणें अन्तःकरण में झांकने लगीं और आत्मा का स्वरूप जाना ही नहीं गया, वरन् उसका लक्ष्य भी माना गया।
आत्मा-परमात्मा की चर्चा वाग् विलास के लिए आये दिन होती रहती है। उसकी सार्थकता तभी है, जब शरीर गत स्वार्थों को सीमित करके आत्म-कल्याण के लिए आवश्यक रीति-नीति अपनाने की आकुलता उभरने लगे।
आत्मा ही विद्या है—
एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया—आचार्य प्रवर विद्या और अविद्या में भेद क्या है? श्वेताश्वतरोपनिषद का आचार्य उत्तर देता है— ‘‘क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या ।’’
हे तात! नाशवान् जड़ पदार्थ हैं वही अविद्या है तथा अविनाशी आत्मा ही विद्या रूप है। सूक्ष्म शरीर—
इसी उपनिषद् में अविनाशी आत्मा की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि—
अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्ध गुणेनात्मगुणेन चैव । आराग्र मात्रो ह्यपरौऽपि दृष्टः ।। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स तिज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पत ।। —श्वेता श्वतरोपनिषद् 5।8-9
अर्थात्—हे तात! वह अंगूठे जितना लघु होकर भी संकल्प-विकल्प युक्त (अर्थात् सोचता विचारता है तथा अपनी बुद्धि के गुण से और श्रेष्ठ कर्मों के गुण से सुई के अग्रभाग जैसे आकार वाला हो गया है ऐसा सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा भी ज्ञानियों ने देखा दे देखा है। बाल के सौवें अंश से भी सौवें अंश परिमाण वाला भाग ही प्राणी का स्वरूप जानना चाहिये वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिमाण वाला आत्मा असीम गुणों वाला हो जाता है।
इन दो ऋचाओं में शास्त्रकार ने जीवन के विराट-दर्शन को सूत्र-रूप में पिरो दिया है। प्रकट है कि शरीर दो प्रकार के परमाणुओं से बनता है एक होते हैं जड़ दूसरे चेतन। जड़ परमाणु चूंकि स्थूल हैं इसलिये वह दिखाई देते हैं किन्तु चेतना एक प्रकार की तरंग, शक्ति और प्रकाश रूप है और देह में इस प्रकार सोखी हुई है जिस प्रकार सूखी मिट्टी का ढेला जल की जज्ब (सोख लेता है कर लेता है। उसके अस्तित्व का प्रमाण बुद्धि है उसी के न रहने पर शरीर सोचने विचारने की क्रियायें बन्द कर देता है। इस शक्ति का सांसारिक प्रयोजनों में खर्च करते रहने से वह नष्ट होती रहती है और जीव छोटा से छोटा (शरीर से भी और योनियों से भी, होता चला जाता है अनेक कल्पित रूपों में वह अनेक शरीरों में तब तक भ्रमण करता रहता है जब तक श्रेष्ठ कर्मों के गुण से वह फिर से शक्ति संचय करता हुआ सूर्य के समान असीम और तेजस्वी नहीं हो जाता। यह भी कहा है कि ज्ञानियों ने उसे देखा है—ज्ञानियों! संबोधन का अर्थ ही है ज्ञान अर्थात् वह ज्ञान से ही देखा जा सकता है। ज्ञान कोई पदार्थ नहीं है वह निरपेक्ष अवस्था है अर्थात् जिस समय पदार्थ, समय, गति और कारण सभी एकाकार हो जाते हैं ध्यान की उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। ध्यान द्वारा ही वह आत्मा अपने प्रकाश रूप में दिखाई देता है।
आज का विज्ञान यों आत्मा के अस्तित्व तक पहुंच गया है पर इसी ध्यान और अनुभूति (ज्ञान) के अभाव में वह इस तत्व को मानने को तैयार नहीं होता। मनुष्य शरीर जिन छोटी-छोटी प्रोटोप्लाज्मा की ईंटों से बना है वह दो भागों में विभक्त है— 1. नाभिक (न्यूक्लियस) 2. साइटोप्लाज्म के अन्तर्गत जल, कार्बन, नाइट्रोजन, आकाश आदि सभी पंच भौतिक ठोस द्रव तथा गैस अवस्था वाले पदार्थ पाये जाते हैं विभिन्न प्राणधारियों का यहां तक कि मनुष्य-मनुष्य के साइटोप्लाज्म में फर्क होता है। यह वंशानुगत आहार पद्धति और जलवायु आदि पर आधारित है और परिवर्तनशील भी है। आहार के नियमों तथा एक स्थान से दूरी जलवायु वाले स्थान में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे शरीरों के स्थूल भाग में अन्तर आ सकता है पर अभी तक चेतन की अर्थात् नाभिक की क्रियाओं पर विज्ञान कोई नियन्त्रण नहीं पा सका अलबत्ता वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि नाभिक में ही मनुष्य की सारी बौद्धिक चेतना काम करती है। उसमें न केवल अमर व अविनाशी गुण सूत्र विद्यमान हैं वरन् वह सूत्र सारे ब्रह्माण्ड को नाप सकने की क्षमता से परिपूर्ण हैं। सारे शरीर में यह चैतन्य तत्व एक शक्ति, एक तरंग की भांति विद्यमान है उसी के न रहने पर शरीर नहीं रहता। यह चेतना ही है जो मनुष्य शरीर से लेकर सृष्टि के स्थूल कणों तक में व्याप्त हो रही है। जहां तक चेतना का अंश प्राकृतिक परमाणुओं से शक्तिशाली होना है यहां तक तो जड़ और चेतन का अन्तर स्पष्ट प्रतीत होता रहता है पर एक अवस्था ऐसी आती है जब जड़ता चेतनता पर पूरी तरह घटाटोप हो जाती है वही अवस्था है जब चेतना पूर्ण रूप से जड़ गुणों वाली अर्थात् कंकड़-पत्थर जैसी स्थिति में चला जाता है। मुख्य रूप से सृष्टि की चेतना एक ही है पर वह गुणों के द्वारा क्रमशः जड़ होती चली गई है जो जितना जड़ हो गया वह उतना ही उपभोग्य हो गया पर जिसने अपनी चेतना का जितना अधिक विकास किया वही उतना उपभोक्ता होता चला जाता है।
विकास शास्त्रियों ने मनुष्य को अन्यान्य जीवों का विकसित रूप बताया है। कहा नहीं जा सकता यह सिद्धान्त कितना सच है। किन्तु उन्होंने एक शरीर से दूसरे शरीर में विकास की जो कड़ियां बैठाई हैं। वह दरअसल सराहनीय और परिश्रम का काम था। इसी सिद्धान्त से आज यह भी पुष्ट किया जा सकता है यह आत्मा ही जड़ व चेतन सर्वत्र गतिशील है पेड़, पौधों को जड़ और चेतन के बीच की नीचे की कड़ी कहा जा सकता है और जीवित-ग्रहों को उच्च कड़ी। यह प्रतिपादन ही जड़ता से असीम चेतनता के विकास का प्रमाण माना जा सकता है।
यह चेतना जड़ में भी जाती है इसका प्रमाण है वृक्ष, वृक्ष को शास्त्रों में जड़ व चेतन की सन्धि योनि माना गया है। यलोस्टोन नेशनल पार्क (अमरीका) में जहां उबलता पानी पृथ्वी से निकलता है वहां पर चारों ओर लाल रंग का किनारा बन गया है। बहुत दिनों तक यह लाल रंग वैज्ञानिकों को हैरान किये रहा। ऐसा किन्हीं जलाशयों के किनारे नहीं मिलता फिर इस लाल रंग का रहस्य क्या है यह जानने के लिये शोध प्रारम्भ हुई तब पता चला कि यह कोई न होकर जीवित पदार्थ है। इतनी तेज गर्मी में जहां कि मनुष्य का हाथ झुलस जाता है, जीवन का अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिये आश्चर्य की तबा थी। इस आश्चर्य में एक और भी आश्चर्य बाद में समझ में आया। वह यह था कि इस जीवित पदार्थ में जीवन और निर्जीवन दोनों के गुण विद्यमान यह है फायलस स्यनोफाइटावर्ग की एक ‘‘अलगी’’ है। सामान्यतः ‘‘अलगी’’ में नीला हरा-सारहीन द्रव्य (पिगमेंट) क्लोरोफिल के साथ रहता है, पर कुछ में लाल रंग का भी द्रव्य होता है।
फायलम यूग्लेनो फाइटा में भी पौधे व जन्तुओं दोनों के गुण पाये जाते हैं। इसमें ‘‘क्लोरोफ्लास्ट’’ (इसी में क्लोरोफिल नामक हरा द्रव्य होता है जो मुख्यतः वृक्षों का गुण है) रहता है, वह इसके पौधा होने का प्रमाण है। लेकिन जिस प्रकार पौधों के कोशों (सेल्स) में दीवार (सेलवाल) होती है, उस तरह की दीवार इनमें नहीं होती। वरन् इनके चारों ओर पहुंचा भोजन इन्जाइम्स के द्वारा पचाया जाता है। इन्जाइम्स ये स्वयं निकालते हैं। यह भोजन अन्धेरे में पचा सकते हैं इनकी वृद्धि भी एक कोश में होती है कोशीय भित्ति (सेलबाल) के स्थान पर इनमें लचीली कोशीय झिल्ली होती है वह ठोस भूमि पर संकुलित होती और फैलती है तो इस क्रिया द्वारा वह चल भी लेती है। इनमें ‘आई स्पॉट’ भी होता है जिससे यह विश्वास किया जाता है कि यह देखते भी हैं। इसके ही पास में एक छिद्रवाहिनी (वेक्यूल) होती है वह पानी व भोजन चूसने तथा निकालने का भी काम करती है वोक्यूल ज्यादातर एक कोशीय जन्तुओं में होता है। इनमें एक जीवधारी के पोषण (न्यूट्रिशन) ग्रहण पचाना (हालिजिक) तथा लैंगिक प्रजनन (सैक्सुअल रिप्रोडम्शन) गुण भी होते हैं। इन सभी उदाहरणों से यह विदित होता है कि जिसे वनस्पति घट माना जाता है। वह भी एक जीव की ही कोई अवस्था है। इस प्रकार धीरे-धीरे अपनी चेतनता के रहे-सहे अंश को छोड़ता हुआ एक दिन पूर्ण जड़ स्थिति में चला जाता है।
जीवात्मा के उच्च श्रेणी विकास का प्रमाण है जीवित ग्रहों में प्लाज्मा की उपस्थिति। पृथ्वी के सभी जीवधारियों के शरीर ठोस और द्रव पदार्थों से बने हैं इन्हीं की एक अवस्था गैस। एक पदार्थ का आयतन जितना सघन होगा वस्तु उतनी ही ठोस होगी पर जितना-जितना वह द्रव तथा गैस रूप में आती जायेगी उसका आयतन बढ़ता जायेगा। ठोस की शक्ति से गैस की शक्ति बड़ी होती है पर गुणों की दृष्टि से गैस में भी ठोस के गुण रहते हैं। वैज्ञानिक अब यह भी मानने लगे हैं कि जीवन केवल ठोस स्थिति में ही नहीं द्रव व गैस की अवस्था में भी रह सकता है। वैज्ञानिकों को वह प्रमाण मिले हैं कि जब पृथ्वी तप्त तवे के समान जल रही थी तब भी एक कोषीय जीव पृथ्वी पर उपलब्ध थे। और जब एक नई शक्ति ‘‘प्लाज्मा’’ के ज्ञान ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि यदि गैस स्थिति में जीवन रह सकता है तो प्लाज्मा में भी रह सकता है। प्लाज्मा ‘‘प्राण शक्ति’’ का वैज्ञानिक नाम है। इसे सूक्ष्म शरीर या प्रकाश शरीर कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार प्लाज्मा कोई विशिष्ट वस्तु न होकर ठोस-द्रव तथा गैस की तरह ही पदार्थ की चौथी-अवस्था है (हिन्दी डाइजेस्ट सन् 1962 अप्रैल अंग पेज 69, आकाश में चमकते हुए तारे प्लाज्मा ही हैं। यह प्लाज्मा एक प्रकार का ईंधन या आहार ही है। तारागण उसे किस प्रकार ग्रहण करके अपना जीवन धारण किये हुए हैं अभी तक वैज्ञानिक यह जानने में समर्थ नहीं हो पाये पर विशिष्ट तत्वों से प्लाज्मा का निर्माण करके उन्होंने यह सिद्ध अवश्य कर दिया है कि जिस प्रकार हमारे शरीरों में नाभिकीय द्रव्य की उपस्थिति से ही साइटोप्लाज्मा का निर्माण होता है उसी प्रकार सितारों में भी नाभिकीय गुण होने चाहिये यदि ऐसा है तो फिर उन्हें भी जीवधारी ही मानना चाहिये जैसा कि भारतीय आर्ष-ग्रन्थों में सूर्य को आत्मा चन्द्रमा पृथ्वी आदि को भी देवता कहा है।
प्लाज्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी अत्यन्त शक्तिशाली पदार्थ है। एक पौण्ड नाइट्रोजन का प्लाज्मा से एक इंजिन पूरे एक वर्ष तक चल सकता है। गैस को अत्यधिक गर्म करने से इलेक्ट्रान तीव्र गति करते हैं और एक परमाणु का इलेक्ट्रान हट कर अलग हो जाता है व अन्य परमाणु आयन बन जाता है। यह आयनी भूत गैस ही प्लाज्मा कहलाती है। आजकल विद्युत तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाई जाती है। पर प्लाज्मा के बारे में ज्ञान से वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि यह विज्ञान जब पूरी तरह विकसित हो जायेगा तो तारों के झंझट से मुक्ति मिल जायेगा तक केवल चुम्बकीय आकर्षण द्वारा कहीं भी शक्ति पैदा कर ली जा सकेगी।
प्लाज्मा एक प्रकार का प्रकाश और ताप युक्त प्राण ही है। मनुष्य शरीर से लेकर अन्य चेतन धारियों में वही शक्ति जीवन का आधार है। इसी शक्ति के पतन से मनुष्य लघुतम बनता है तो इसी के विकास से वह सूर्य जैसी महान् गुणों वाली चेतना में अपना विकास करके विराट बन जाता है। इसी का नाम विद्या है इस विद्या की प्राप्ति के लिये भारतीय आचार्यों ने अनेक साधनायें विकसित की हैं। प्लाज्मा की शक्ति से ही अनुमान किया जा सकता कि आत्म-शक्ति के सूक्ष्म या प्रकाशीय विकास द्वारा मनुष्य कितना समर्थ व शक्तिशाली बन सकता है। जबकि आज का विज्ञान केवल जड़ की व्याख्या और उसी को यांत्रिक नियंत्रण में लगा है यही अविद्या है। अविद्या को हटाकर विद्या की प्राप्ति कर सकें तो शास्त्रकार के कथन के अनुसार अंगुष्ठ मात्र प्राणी सूर्य जैसा विराट् बन सकता है।
वहां न वर्ण भेद है न लिंग भेद
आत्मा के पशु पक्षियों, वृक्ष वनस्पति में भी होने की बात पर कितने विवाद हैं कहा नहीं जा सकता। इसका एक ही कारण है कि कोई भी दर्शन आत्म-सत्ता का सर्व सफल हल प्रस्तुत नहीं कर सका। अनुभूत और प्रायोगिक दर्शन होने के कारण इस प्रश्न को ही भारतीय योग विज्ञान ही सुलझाता रहता है एक ही वस्तु का अनेक रूपों में रूपान्तर किसी समय में समझ में न आने वाली बात हो सकती है पर आज तो वैज्ञानिक पदार्थ के स्थूल, हवा, वायु भूत तथा प्लाज्मा अनेक स्वरूप जान गये हैं। अतएव रूपान्तर कोई सयस्दा नहीं रही। फिर भी आत्मा नर है या नारी यह प्रश्न अक्सर उठता रहता है। तात्विक दृष्टि से प्रश्न में कोई वजन न होने पर भी जिज्ञासा का समाधान आवश्यक समझा गया।
आत्मा का आस्तित्व
आत्मा न नर है न नारी। वह एक दिव्य सत्ता भर है। समयानुसार—आवश्यकतानुसार वह तरह-तरह के रंग-बिरंगे परिधान पहनती बदलती रहती है। इसी को लिंग व्यवस्था समझना चाहिए। सर्दी की ऋतु में गरम और भारी कपड़े पहनने की आवश्यकता अनुभव होती है और गर्मी में हलके वस्त्र पहनने या नंगे रहने की इच्छा होती है। नर-मादा रूपों दो आवरण दो ऋतुओं के लिए हैं। आत्मा की जब जैसी रुचि होती है तब वह वैसे वस्त्र पहन लेता है। कभी गरम भारी कभी ठंडे—झीने। कभी खट्टा स्वाद चखने की इच्छा होती है कभी मीठा।
दामा के जीवन का अपना आनन्द है और अपना स्तर उसे देखे समझे और अनुभव किये बिना आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सो जब स्नेह वात्सल्य, समर्पण सेवा की प्रवृत्तियां उभारने की शिक्षा लेनी होती है तो नारी के शरीर में प्रवेश करके उस तरह का अध्ययन, अनुभव, अभ्यास करना होता है और जब शौर्य, साहस, पुरुषार्थ श्रम की कठोरता का शिक्षण आवश्यक होता है तब उसे नर कलेवर पहनना पड़ता है।
मृदुलता और कठोरता के उभयपक्षीय समन्वय से जीवधारी की समग्र शिक्षा हो पाती है यदि वह एक ही योनि में पड़ा रहे तो उसके आधे ही गुणों का विकास हो पायेगा और उस अपूर्णता के रहते सर्वांगीण पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा। अस्तु भगवान ने यह व्यवस्था बना रखी है कि जीवधारी कभी मादा शरीर में रहा करे कभी नर में। यह परिवर्तन धूप-छांह जैसे उभयपक्षीय आनन्द की अनुभूति कराता है और जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित ही नहीं अभ्यस्त भी रखता है।
यह सोचना ठीक नहीं कि नर जन्म-जन्मांतरों तक नर ही रहेगा और नारी को नारी ही रहना पड़ेगा। अभ्यास और रुचि परिपक्व हो जाय तो एक ढर्रा भी कई जन्मों तक चलता रह सकता है, पर यदि तीव्र उत्सुकता उत्कंठा हो तो वह परिवर्तन अगले ही जन्म में हो सकता है। नर यदि नारी जैसी मनोभूमि और गतिविधियां अपना कर उस तरह की उत्कण्ठा तीव्र करे तो अगला जन्म उसे नारी के रूप में भी मिल सकता है इसी प्रकार नारी के लिए यह सर्वथा सम्भव है कि वह पुरुषोचित गतिविधियां और मनोवृत्तियां अपनाकर अगला परिवर्तन अपनी अभिलाषा के अनुरूप करले। यों प्रकृति के नियमानुसार बिना किसी प्रयत्न के भी यह परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर शास्त्री यह तथ्य भली प्रकार जान गये हैं कि हर जीवधारी में नर और नारी की उभयपक्षीय सत्ता बीज रूप में विद्यमान रहती है। उसका जो पहलू उभरा रहता है उसी को समर्थ एवं सक्रिय रहने का अवसर मिलता है—और दूसरा पक्ष प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। यदि उभार दूसरी दिशा में वह निकले तो सुप्त पक्ष जागृत हो सकता है और जागृत को सुषुप्ति में चला जाना पड़ता है।
सृष्टि में ऐसे अगणित जीवधारी विद्यमान हैं जिनमें नर और नारी के दोनों पक्ष समान रूप से सक्रिय होते हैं। वे एक ही जीवन में कभी नर और कभी मादा बनते रहते हैं। जब उनका जी आता है अपने संकल्पबल से नर बन जाते हैं और जब उमंग उठती है नारी स्वभाव ही नहीं बिना किसी कठिनाई के नारी अंगों का भी विकास अधूरा नहीं होता, वरन् इस सीमा तक प्रखर होता है कि सन्तानोत्पादन भी भली प्रकार से हो सके। आज का नर कल नारी बन कर अपने पेट में गर्भ धारण करेगा और परसों बच्चे जनेगा यह बात विचित्र लगती है, पर है सर्वथा सत्य कितने जीवों में यही प्रवृति है और वे एक ही जीवन में इस प्रकार के उभय-पक्षीय आनन्द की अनुभूतियां लेते रहते हैं। उनके जीवन समुद्र में कभी नर का ज्वार आता है तो कभी नारी का भाटा। प्रकृति ने उन्हें इच्छानुसार आवरण बदलने की जो सुविधा दी है वैसी ही यदि मनुष्यों को भी मिली होती तो वे भी इस प्रकार का आनन्द, लाभ करते। इतना ही नहीं नर और नारी के बीच असमानता की जो खाई बन गई है उसके बनने का कोई कारण न रहता। फिर न कोई छोटा समझा जाता न कोई बड़ा। किसी को किसी पर आधिपत्य जमाने की खुराफात भी न सूझती।
गोल्ड इस्मिट, रोश, हरीसन आदि प्राणि वेत्ताओं ने तितलियों की कलम एक दूसरे को लगा कर उनका लिंग परिवर्तन कृत्रिम रूप से सम्भव बना कर दिखाया है। विज्ञानी डबल्यू. हीरम्स ने मछलियों की कई जातियां उभयलिंगी पाई है और कुछ प्रयोगों में छोटे आपरेशन करके उन्हें परिवर्तित लिंग का बनाया है। पक्षियों में भी लिंग परिवर्तन के आपरेशन बड़ी मात्रा में सफल हुये हैं।
कुछ कीड़े होते हैं जो एक ही शरीर में बार-बार उभय लिंगी परिवर्तन करते रहते हैं। वे कभी नर बन जाते हैं कभी मादा। कीट विज्ञानी प्रो. ओरटन ने ऐसे जीवों की खोज की थी जो एक ही जन्म में कभी नर रहते हैं कभी नारी। ओइस्टर ऐसे जन्तुओं में अग्रणी हैं। वे मादा की तरह अण्डे देने के बाद ही नर बन जाते हैं। और उभयपक्षीय लिंग में रहने वाली विभिन्नताओं का आनन्द लूटते हैं। आस्ट्रिना गिवासा, स्लग लाइयेकस जाति के जलचर भी उभयलिंगी रसास्वादन का क्रम परिवर्तन करते रहते हैं लिमेष्ट्रिया पतंगा भी इसी स्तर का है वह कभी नारी होता है तो कभी नर।
आयस्टर वर्ग-जाति का ‘मोलस्क’ घोंघा अपने लिंग परिवर्तन करता रहता है। कभी वह मादा होता है तो कभी नर। 40 साल की पूरी आयु यदि वह जी सके तो प्रायः एक दर्जन बार वह अपना लिंग परिवर्तन करता है।
सृष्टि में ऐसे जीव-जन्तुओं की संख्या कम नहीं जो उभयलिंगी होते हैं। एक ही शरीर में शुक्र और डिम्ब उत्पन्न करने वाली ग्रन्थियां होती हैं। जब उनमें प्रौढ़ता आती है तो प्रजनन स्राव आप प्रवाहित होते हैं और रक्त संसार के सहारे उनको आत्मरति का आनन्द प्रजनन का लाभ मिल जाता है। ड्रोसोफिला मक्खी हैव्रो ब्रेकन ततैये, सिल्क व्रम मोथ, वैनस मोथ, जिप्सी मोथ, ओलोकेसपिस जैसे अनेक पतंगे उभयलिंगी होते हैं।
समझा जाता है कि नर और मादा का संयोग होना सन्तानोत्पादन के लिए आवश्यक है। पर यह मान्यता बड़े आकार वाले विकसित जीवों पर ही एक सीमा तक लागू होती है। छोटे जीवों में अगणित जातियां ऐसी हैं जिनमें प्रजनन के लिए साथी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने शरीर में रहने वाली उभय योनियां समयानुसार स्वयं ही संयोग बना लेती हैं और उस आत्मरति से ही प्रजनन का अध्याय पूरा हो जाता है।
प्रजनन क्रिया के लिए यौन संयोग के अतिरिक्त एक और भी तरीका है अपने विकसित स्वरूप को विघटित कर देना ‘‘यह क्रिया वनस्पति जगत में ही निरन्तर होती है। बीज गलकर अंकुर और पत्र पल्लवों के रूप में विकसित होता है और एक से अनेक बनने का क्रम अपना कर कालान्तर में वही पुष्ट पौधा बनकर कितने ही नये बीज हर साल उत्पन्न करता है। यह अमैथुनी प्रजनन क्रिया वनस्पति जगत का सर्व विदित परिपाटी है।
गन्ना, गुलाब आदि अगणित पौधे उनके टुकड़े करके गाढ़ देने पर अलग-अलग पौधे बन जाते हैं। वट गूलर जैसे वृक्षों की बड़ी डालियां भी नये पेड़ का रूप धारण करती हैं विकसित पुष्पों के पराग हवा में उड़ कर एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। मक्खियां और तितलियां भी उनका स्थानान्तर करती रहती हैं इस प्रकार पराग युगल परस्पर योग संयोग मिलाकर बिना रति क्रिया के अपनी वंश वृद्धि करते रहते हैं।
छोटे जीवों में भी वह गुण होता है कि वे अपने शरीर से अपने ही सरीखी नई संतति उत्पन्न कर सकें। यों दूसरी जाति की उत्पत्ति तो सहज ही हो जाती है। पेट में सड़ा अन्न मलकृमि बनकर विष्ठा के साथ निकलता है शरीर पर चिपका हुआ मैल जुए, चीलर बनता है, जीवित या मृत शरीर का सड़ा हुआ मांस आंख से देखे जा सकने वाले कीड़ों के रूप में अनायास ही बदल जाता है। सड़े हुए फल और तरकारियों में भी उसी रंग रूप के कीड़े रेंगते देखे जा सकते हैं। यह प्रजनन ही है। सड़न को रतिक्रिया तो नहीं कह सकते और न उससे सहधर्मी जीव उत्पन्न होता है फिर भी इसे जीव उत्पादन तो कह ही सकते हैं। कीचड़ और गन्दगी में मक्खी, मच्छरों और रेंगने वाले कृमियों का उत्पन्न होना इसी स्तर का प्रजनन है।
जिनकी गणना जीवधारियों में की जाती है ऐसे प्राणी भी अपने शरीर के ही टुकड़े बखेर कर अपनी जाति के नये प्राणी को जन्म देकर विधिवत वंश वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए उन्हें जाड़ा ढूंढ़ने या रति-क्रिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना शरीर ही इसके लिये पर्याप्त होता है और उसी से उभयपक्षीय मिलन संयोग से लेकर प्रजनन तक की सारी आवश्यकतायें सुचारु रूप में सम्पन्न होती रहती हैं। ‘अमीबा’ और ‘डायटम’ जीव इसी स्तर के हैं। उनमें जब प्रौढ़ता आती है तो अपनी ही शरीर को फुला कर उसका भाग अलग छिटका देते हैं और वह एक स्वतन्त्र प्राणी बनकर अपनी अलग वंश परम्परा का संचालन करता है।
जीवित कहे जाने वाले प्रत्येक जीवधारी या जीवाणु में मेटाबोलिज्य उपापच्य प्रजनन शक्ति होती है। सृष्टि में जीवधारियों का उत्पादन अभिवर्धन कैसे उत्पन्न हुआ इसका युक्ति संगत एक मात्र उत्तर यही हो सकता है कि आदि जीवाणुओं में अपने आपको विखण्डित करने सन्तानोत्पादन करने की सरलतम योग्यता विद्यमान थी। उसी के आधार पर जीवधारियों की संख्या बढ़ी और परिस्थितियों के अनुरूप उनने अपनी काया तथा चेतना का विकास परिष्कार किया। रतिक्रिया का प्रचलन तो बहुत बाद में—तब हुआ-जब प्राणधारी एक लिंगी न रह कर द्विलिंगी बन गये और उन नर-मादा की जननेन्द्रियां स्पष्ट उभरीं तथा गर्भ धारण के योग्य हो गई। इससे पूर्व अपने शरीर से विखण्डित होकर ही पीढ़ियां बढ़ाने का प्रचलन था। इसके आगे-मध्यकाल-में उभयलिंगी अन्तःस्राव मात्र उभय और पुष्प-पराग की तरह जीवधारी नर-मादा परस्पर स्नेह आलिंगन का क्रिया-कलाप गन्ध मादकता के आधार पर करने लगे थे। उतने से ही उनमें प्रजनन उपयोगी हलचलें उठ खड़ी होती थीं और सन्तान होने लगती थी यौन संसर्ग तो बहुत बाद की प्रगतिशीलता है।
सेलों के भीतर भरे न्यूक्लिक ऐसिड के माध्यम से पूर्वजों की शारीरिक, मानसिक विशेषतायें सन्तान में हस्तान्तरित होती है। एडमोसिन फास्टेट रसायन का होना प्रजनन योग्यता के लिए आवश्यक है। इन तत्वों को यदि प्राणियों में घटाया-बढ़ाया जा सके तो उनकी प्रजनन क्षमता का स्तर भी बदल सकता है। यह असम्भव नहीं कि क्षुद्र जीव अनभ्यस्त रतिक्रिया अपनाने लगे और सुविकसित प्राणी जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, अकेला—बिना सहचर के—बिना रति-क्रिया के सुयोग्य सन्तान का उत्पादन कर सकें।
पेप्टाइड रसायन का यह विदित गुण है कि गरम करने पर वह पानी में घुलता है और ठण्डा होने पर छोटे पिण्ड की शकल धारण कर लेता है। बाहर से उपयुक्त रासायनिक भोजन मिले और उपयुक्त ऊर्जा का वातावरण मिले तो उनमें विभाजन प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। इसी आधार पर जीवशास्त्री कृत्रिम जीवाणु उत्पन्न करने और उनसे वंश-वृद्धि का उपक्रम आरम्भ कराने के लिए प्रयत्नशील है।
आये दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिनमें नर के भीतर नारी के अथवा नारी के भीतर नर के यौन चिह्न विकसित होते चले गये और स्थिति यहां तक जा पहुंची की आपरेशन करके उनका लिंग परिवर्तन करना पड़ा। यह परिवर्तन इतना सफल रहा कि उन्होंने जोड़ा बनाया और सफल दाम्पत्य जीवन जीते हुए सन्तानोत्पत्ति भी की। मनोविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के आधार पर यह सिद्धान्त मान्यता प्राप्त है कि लिंग परिवर्तन के लिए मानवी प्रयत्न बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन तो इस जन्म में भी हो सकते हैं अन्यथा अगले जन्म में तो वह सम्भावना शत-प्रतिशत साकार हो सकती है। पुराणों में इस प्रकार के अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें व्यक्तियों ने अपने संकल्प बल एवं साधना उपक्रम के द्वारा लिंग परिवर्तन में सफलता प्राप्त की है इन दिनों भले ही वे उपचार विस्मृत विलुप्त हो गये हों—इससे क्या—तथ्य तो जहां के तहां ही रहेंगे। आत्मा के सुदृढ़ संकल्प और प्रयत्न यदि प्रखर होवें तो किसी भी आत्मा के लिए अपना वर्तमान लिंग बदल लेने की पूरी पूरी सम्भावना हो सकती है।
कभी कभी किन्हीं पुरुषों में नारी प्रकृति और नारियों में पुरुष प्रकृति पाई जाती है। उनके हाव-भाव स्वभाव एवं आचरण में इस प्रकार का अन्तर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसका एक मात्र कारण यह है कि पिछले दिनों उनकी मन्द इच्छा लिंग परिवर्तन की तो रही पर उनमें प्रौढ़ता प्रखरता नहीं आई। यदि उनका संकल्प बल और प्रयत्न बलशाली रहा होता तो उन्हें इस प्रकार के आधे अधूरे परिवर्तन का सामना न करना पड़ता। इतने पर भी उनका प्रवृत्ति परिवर्तन की दिशा में ही मन चलता रहे तो यह आशा की जा सकती है कि इस विराम के उपरान्त वे अपनी अभीष्ट मनोवांछा के अनुरूप लिंग परिवर्तन का लक्ष्य अगले जन्म तक पूरा कर लेंगे।
कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें पुरुष के शरीर से भी बच्चों का जन्म हुआ है। भले ही वे भ्रूण अविकसित रहे हों और भले ही वे जुड़वा भाई समझे जा सकते हों पर उत्पत्ति तो नर शरीर से हो ही गई। इन उदाहरणों से यह तो सिद्ध होता ही है कि मात्र नारी के शरीर में ही नहीं—नर कलेवर में भी वह क्षमता मौजूद है कि गर्भ धारण करने से लेकर गर्भपोषण तक कि क्रिया सम्पादन कर सके। अवसर मिले तो इस सम्भावना का अधिक विकास भी हो सकता है ओर नारी की तरह ही नर भी प्रजनन कर्म कर सकने में समर्थ हो सकते हैं।
फ्रांस के एक 17 वर्षीय लड़के जीन जक्यूस लोरेन्ट को छाती के दर्द की शिकायत थी। डाक्टरों ने फेफड़े का ट्यूमर पाया और उसका आपरेशन किया, डाक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने ट्यूमर के स्थान पर 3 पौण्ड 15 ओंस वजन का एक विकसित अंगों वाला बच्चा निकाला।
ब्रिटिश पैथोलोजिस्ट ऐसोशियेशन ने एक भ्रूण को लड़के का जुड़वा भाई बताया है जो गर्भ-काल में किसी प्रकार उसके शरीर में प्रवेश कर गया और वही बढ़ता पलता रहा।
इसी प्रकार की एक घटना बरेली (उ. प्र.) के जिला अस्पताल में हुई। बदायूं निवासी एक दो वर्ष के बालक का आपरेशन पेट का ट्यूमर समझ कर किया गया पेट खोलने पर उसमें एक विकसित भ्रूण पाया गया। जिसे अधिक अन्वेषण के लिए सुरक्षित रख लिया गया।
नर के शरीर से बच्चे की उत्पत्ति की अनेकों घटनायें बहुचर्चित हैं और उनके विवरण पत्र पत्रिकाओं में विस्तार पूर्वक छपे हैं। सन् 1956 में टोक्यो अस्पताल में एक किशोर लड़के के पेट का आपरेशन करके उसमें से 11 ओंस का अपरिपक्व बच्चा निकाला था। बच्चे की टांगें, बाल एवं शरीर के अन्य भाग स्पष्ट थे। उसी साल सन् 1956 में उत्तर वियतनाम के हनोई अस्पताल में एक पुरुष का आपरेशन करके बच्चा निकाला था जो जन्मते समय रोया भी था।
सन् 1954 में पाकिस्तान के बहाबलपुर नगर के विक्टोरिया अस्पताल में डाक्टरों ने एक पुरुष का पेट चीर कर उसमें बच्चा निकाला था।
इन तथ्यों पर गहराई से विचार किया जाय तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि नर और नारी के कलेवर करती और बदलती रहने पर भी आत्मा की स्थिति दोनों से ऊपर है अथवा उभयपक्षीय सम्भावनाओं से भरपूर है। जो आज नर है कल नारी बनना पड़ सकता है। इसी प्रकार नारी को नर की भूमिका सम्पादित करने का अवसर भी मिलता है। जब यह आवरण सामयिक है। तो नर और नारी के बीच ऐसी दीवारें क्यों की जायं जिनमें अधिकार और कर्तव्य की खाई खड़ी की जाय। किसी को छोटा, किसी को बड़ा माना जाय। दोनों को मिलजुल कर ऐसी समाज व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे बदलते रहने वाली लिंगीय परिस्थिति में किसी आत्मा को असुविधा अथवा अन्याय का अनुभव न करना पड़े।
यह युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने अदृश्य, अप्रकट को स्पष्ट करने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है सच पूछा जाये तो उसने भारतीय दर्शन के आत्मावादी सिद्धान्त को पूरी तरह पुष्ट भी कर दिया है किन्तु प्रायः विज्ञान जिन के पास है उन्हें आध्यात्म दर्शन के सामीप्य का अवसर नहीं मिला अतएव सूक्ष्म का तथ्यान्वेष कर लेने के बावजूद वैज्ञानिकों के सम्मुख भी यह प्रश्न उलझा का उलझा रहा गया। इसे इस युग की एक अद्भुत उपलब्धि कहा जाना चाहिए कि मानवीय अन्तःकरण ने विज्ञान की संगति आध्यात्म से मिलाकर इस महत्व पूर्ण प्रश्न को सुलझाने का यत्न किया।
मैं और मेरे में उलझी सचाई
मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? इन छोटे से प्रश्न का सही समाधान न कर सकने के कारण ‘मैं’ को कितनी कितनी विषम विडम्बनाओं में उलझना पड़ता है और विभीषिकाओं में संत्रस्त होना पड़ता है, यदि यह समय रहते समझा जा सके तो हम वह न रहें, जो आज है। वह न सोचें जो आज सोचते हैं वह न करें जो आज करते हैं। हम कितने बुद्धिमान हैं कि धरती आकाश का चप्पा-चप्पा छान डाला और प्रकृति के रहस्यों को प्रत्यक्ष करके सामने रख दिया। इस बुद्धिमत्ता की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम और अपने आपके बारे में जितनी उपेक्षा बरती गई उसकी उतनी निन्दा की जाय वह भी कम ही है।
जिस काया को शरीर समझा जाता है क्या यही मैं हूं? क्या कष्ट, चोट, भूख, शीत, आतप आदि से पग-पग पर व्याकुल होने वाला अपनी सहायता के लिए बजाज, दर्जी, किसान, रसोइया, चर्मकार, चिकित्सक आदि पर निर्भर रहने वाला ही मैं हूं? दूसरों की सहायता के बिना जिसके लिए जीवन धारण कर सकना कठिन हो—जिसकी सारी हंसी-खुशी और प्रगति दूसरों की कृपा पर निर्भर हो, क्या वही असहाय, असमर्थ, मैं हूं? मेरी आत्मा निर्भरता क्या कुछ भी नहीं है? यदि शरीर ही मैं हूं तो निस्सन्देह अपने को सर्वथा पराश्रित और दीन दुर्बल ही माना जाना चाहिए।
परसों पैदा हुआ, खेल कूद, पढ़ने-लिखने में बचपन चला गया। कल जवानी आई थी। नशीले उन्माद की तरह आंखों में, दिमाग में छाई रही। चंचलता ओर अतृप्ति से बेचैन बनाये रही। आज ढलती उम्र आ गई। शरीर ढलने गलने लगा। इन्द्रियां जवाब देने लगीं। सत्ता बेटे, पोतों के हाथ चली गई। लगता है एक उपेक्षित और निरर्थक जैसी अपनी स्थिति है। अगली कल यही काया जरा जीर्ण होने वाली है। आंखों में मोतियाबिन्द, कमर घुटनों में दर्द खांसी, अनिद्रा जैसी व्याधियां, घायल गधे पर उड़ने वाले कौए की तरह आक्रमण की तैयारी कर रही हैं। अपाहिज और अपंग की तरह कटने वाली जिंदगी कितनी भारी पड़ेगी। यह सोचने को जी नहीं चाहता वह डरावना और घिनौना दृश्य एक क्षण के लिए भी आंखों के सामने आ खड़ा होता है तो रोम-रोम कांपने लगता है? पर उस अवश्यंभावी भवितव्यता से बचा जाना सम्भव नहीं? जीवित रहना है तो इसी दुर्दशा ग्रस्त स्थिति में पिसना पड़ेगा। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। क्या यही मैं हूं? क्या इसी निरर्थक विडम्बना के कोल्हू के चक्कर काटने के लिए ही ‘मैं’ जन्मा? क्या जीवन का यही स्वरूप है? मेरा अस्तित्व क्या इतना ही तुच्छ है।
आत्म चिन्तन कहेगा—नहीं-नहीं-नहीं। आत्मा इतना हेय और हीन नहीं हो सकता। वह इतना अपंग और असमर्थ-पराश्रित और दुर्बल कैसे होगा? यह तो प्रकृति के पराधीन पेड़-पौधों जैसा—मक्खी, मच्छरों जैसा जीवन हुआ। क्या इसी को लेकर-मात्र जीने के लिए मैं जन्मा। सो भी जीना ऐसा जिसमें न चैन, न खुशी, न शान्ति, न आनन्द, न सन्तोष। यदि आत्मा—सचमुच परमात्मा का अंश है तो वह ऐसी हेय स्थिति में पड़ा रहने वाला हो ही नहीं सकता। या तो मैं हूं ही नहीं। नास्तिकों के प्रतिपादन के अनुसार या तो पांच तत्वों के प्रवाह में एक भंवर बबूले जैसी क्षणिक काया लेकर उपज पड़ा हूं और अगले ही क्षण अभाव के विस्मृति गर्त में समा जाने वाला हूं। या फिर कुछ हूं तो इतना तुच्छ और अपंग हूं जिसमें उल्लास और सन्तोष जैसा—गर्व और गौरव जैसा—कोई तत्व नहीं है। यदि मैं शरीर हूं तो—हेय हूं। अपनी लिए और इस धरती के लिए भारभूत हूं। पवित्र अन्न को खाकर घृणित मल में परिवर्तन करते रहने वाले—कोटि-कोटि छिद्रों वाले इस कलेवर से दुर्गन्ध और मलीनता निसृत करते रहने वाला—अस्पर्श्य—घिनौना हूं ‘मैं’। यदि शरीर हूं तो इससे अधिक मेरी सत्ता होगी भी क्या?
मैं यदि शरीर हूं तो उनका अन्त क्या है? लक्ष्य क्या है? परिणाम क्या है?—मृत्यु—मृत्यु—मृत्यु। कल नहीं तो परसों वह दिन तेजी से आंधी तूफान की तरह उड़ता उमड़ता चला आ रहा है, जिसमें आज की मेरी यह सुन्दर सी काया—जिसे मैंने अत्यधिक प्यार किया—प्यार क्या जिसमें पूरी तरह समर्पित हो गया—धुल गया। अब वह मुझसे विलग हो जायगी। विलग ही नहीं अस्तित्व भी गंवा बैठेगी। काया में घुला हुआ ‘मैं’—मौत के एक ही थपेड़े में कितना कुरूप—कितना विकृत—कितना निरर्थक—कितना घृणित हो जायगा कि उसे प्रिय परिजन तक—कुछ समय और उसी घर में रहने देने के लिए सहमत न होंगे जिसे मैंने ही कितने अरमानों के साथ—कितने कष्ट सह कर बनाया था। क्या यही मेरे परिजन हैं? जिन्हें लाड़ चाव से पाला था। अब ये मेरी इस काया को—घर में से हटा देने के लिए—उसका अस्तित्व सदा के लिए मिटा देने के लिए क्यों आतुर हैं? कल वाला ही तो मैं हूं।
मौत के जरा से आघात से मेरा स्वरूप यह कैसा हो गया। अब तो मेरी मृत काया—हिलती डुलती भी नहीं—बोलती, सोचती भी नहीं? अब तो उसके कुछ अरमान भी नहीं हैं। हाय, यह कैसी मलीन दयनीय, घिनौनी बनी जमीन पर लुढ़क रही है। अब तो यह पलंग बिस्तर पर सोने तक का अधिकार खो बैठी। कुशाओं बान से ढकी—गोबर से लिपी गीली भूमि पर यही पड़ी है। अब कोई चिकित्सक भी इसका इलाज करने को तैयार नहीं। कोई बेटा, पोता गोदी में नहीं आता। पत्नी छाती तो कूटती है पर साथ सोने से डरती है। मेरा पैसा—मेरा वैभव—मेरा सम्मान हाय रे सब छिन गया—हाय रे मैं बुरी तरह लुट गया। मेरे कहलाने वाले लोग ही—मेरा सब कुछ छीन कर मुझे इस दुर्गति के साथ घर से निकाल रहे हैं। क्या यही अपनी दुर्दशा कराने के लिए मैं जन्मा? यही है क्या मेरा अन्त—यही था क्या मेरा लक्ष्य, यही है क्या मेरी उपलब्धि। जिसके लिए कितने अरमान संजोये थे, जिसके लिए कितने पुरुषार्थ किये थे—क्या उसका निष्कर्ष यही हूं? यही हूं मैं—जो मुर्दा बना पड़ा हूं और लकड़ियों की चिता में जल कर अगले ही क्षण अपना अस्तित्व सदा के लिए खोने जा रहा हूं।
लो अब पहुंच गया मैं चिता पर। लो, मेरा कोमल मखमल जैसा शरीर—जिसे सुन्दर, सुसज्जित, सुगन्धित बनाने के लिए घण्टों श्रृंगार किया करता था, अब आ गया अपनी असली जगह पर। लकड़ियों का ढेर—उसके बीच दबाया दबोचा हुआ मैं!लो यह लगी आग। लो, अब मैं जला। अरे मुझे जलाओ मत। इन खूबसूरत हड्डियों में मैं अभी और रहना चाहता हूं, मेरे अरमान बहुत हैं, इच्छायें तो हजार में से एक भी पूरी नहीं हुई। मुझे मरी उपार्जित सम्पदाओं से अलग मत करो, प्रियजनों का वियोग मुझे सहन नहीं। इस काया को जरा सा कष्ट होता था तो चिकित्सा, उपचार मैं बहुत कुछ करता था। इस काया को इस निर्दयता पूर्वक मत जलाओ। अरे स्वजन और मित्र कहलाने वाले लोगों—इस अत्याचार से मुझे बचाओ। अपनी आंखों के आगे ही मुझे इस तरह जलाया जाना तुम देखते रहोगे। मेरी कुछ भी सहायता न करोगे अरे यह क्या—बचाना तो दूर उलटे तुम्हीं मुझ में आग लगा रहे हो। नहीं—नहीं मुझे जलाओ मत—मुझे मिटाओ मत। कल तक मैं तुम्हारा था—तुम मेरे थे—आज ही क्या हो गया जो तुम सबने इस तरह मुझे त्याग दिया? इतने निष्ठुर तुम सब क्यों बन गये? मैं और मेरा संसार क्या इस चिता की आग में ही समाप्त हुआ? सपनों का अन्त—अरमानों का विनाश—हाय री चिता—हत्यारी चिता, तू मुझे छोड़। मरने का जलने का मेरा जरा भी जी नहीं है। अग्नि देवता, तुम तो दयालु थे। सारी निर्दयता मेरे ही ऊपर उड़ेलने के लिए क्यों तुल गये?
लो, सचमुच मर गया। मेरा काया का अन्त हो ही गया। स्मृतियां भी धुंधली हो चलीं। कुछ दिन चित्र फोटो जिसे। श्राद्ध तर्पण का सिलसिला कुछ दिन चला। दो तीन पीढ़ी तक बेटे पोतों का नाम याद रहे। पचास वर्ष भी पूरे न हो पाये कि सब जगह से नाम निशान मिट गया। अब किसी को बहुत कहा जाय कि इस दुनिया में ‘मैं’ पैदा हुआ था। बड़े अरमानों के साथ जिया था जीवन को बहुत संजोया, संभाला था, उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर वह सारी दौड़, धूप ऐसे ही निरर्थक चली गई। मेरा काया तक ने मेरा साथ न दिया—जिसमें मैं पूरी तरह घुल गया था। जिस काया के सुख को अपना सुख और जिसके दुख को अपना दुख समझा। सच तो यह है कि मैं ही काया था—और काया ही मैं था हम दोनों की हस्ती एक हो गई थी, पर यह क्या अचंभा हुआ, मैं अभी मौजूद हूं।
वायुभूत हुआ आकाश में मैं अभी भी भ्रमण कर रहा हूं। पर वह मेरी अभिन्न सहचरी लगने वाली काया न जाने कहां चली गई। अब वह मुझे कभी नहीं मिलेगी क्या? उसके बिना मैं रहना नहीं चाहता था रह नहीं सकता था, पर हायरी निर्दय नियति। तू ने यह क्या कर डाला। काया चली गई। माया चली गई। मैं अकेला ही वायु भूत बना भ्रमण कर रहा हूं। एकाकी-नितान्त एकाकी। जब काया ने ही साथ छोड़ दिया तो उसके साथ जुड़े हुए परिवारी भी क्या याद रखते—क्यों याद रखते? याद रखे भी रहे हों तो अब उससे अपना बनना भी क्या है?
मैं काया हूं। यह जन्म के दिन से लेकर—मौत के दिन तक मैं मानता रहा। यह मान्यता इतनी प्रगाढ़ थी कि कथा पुराणों की चर्चा में आत्मा काया की प्रथकता की चर्चा आये दिन सुनते रहने पर भी गले से नीचे नहीं उतरती थी। शरीर हो तो मैं हूं—उससे अलग मेरी सत्ता भला किस प्रकार हो सकती है? शरीर के सुख-दुख के अतिरिक्त मेरा सुख-दुख अलग क्योंकर होगा? शरीर के लाभ में अन्तर कैसे माना जाय? यह बातें न तो समझ में आती थीं ओर न उन पर विश्वास जमता था। परोक्ष पर प्रत्यक्ष कैसे झुठलाया जाय? काया प्रत्यक्ष है—आत्मा अलग है, उसके स्वार्थ, सुख दुख अलग हैं, यह बातें कहने सुनने भर की ही हो सकती हैं। सो रामायण गीता वाले प्रवचनों की हां में हां तो मिलाता रहा पर उसे वास्तविकता के रूप में कभी स्वीकार न किया।
पर आज देखता हूं कि वह सचाई थी जो समझ में नहीं आई और वह झुठाई थी जो सिर पर हर घड़ी सवार रही। शरीर ही मैं हूं। यही मान्यता—शराब की खुमारी की तरह नस-नस में भरी रही। बोतल छानता रहा तो वह खुमारी उतरती भी कैसे? पर आज आकाश में उड़ता हुआ वायुभूत—एकाकी—‘मैं’ सोचता हूं। झूठा जीवन जिया गया। झूठ के लिए जिया गया, झूठे बनकर जिया गया। सचाई आंखों से ओझल ही बनी रही। मैं एकाकी हूं, शरीर से भिन्न हूं। आत्मा हूं। यह सुनता जरूर रहा पर मानने का अवसर ही नहीं आया। यदि उस तथ्य को जाना ही माना भी होता तो वह अलभ्य अवसर जो हाथ से चला गया, इस बुरी तरह न जाता। जीवन जिस मूर्खतापूर्ण रीति-नीति से जिया वैसा न जिया जाता।
शरीर मेरा है—मेरे लिए है, मैं शरीर नहीं हूं। यह छोटी सी सचाई यदि समय रहते समझ में आ गई होती तो कितना अच्छा होता। तब मनुष्य जीवन जैसे सुरदुर्लभ सौभाग्य का लाभ लिया गया होता, पर अब क्या हो सकता है। अब तो पश्चात्ताप ही शेष है। भूल भरी मूर्खता के लिए न जाने कितने लम्बे समय तक रुदन करना पड़ेगा?
शरीर ही नहीं आत्मा को भी देखें
शरीर और आत्मा की प्रथकता को जानते बहुत हैं, पर मानते कोई-कोई ही हैं। मरने के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है, इसे प्रत्येक धर्मावलम्बी मानता है। हिन्दू—धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता को पूरी तरह स्वीकार किया गया है। ईसाई, मुसलमान पुनर्जन्म तो नहीं मानते पर मरणोत्तर जीवन स्वीकार करते हैं। शरीर न रहने पर भी आत्माओं का बना रहना और ब्रह्म-लोक में प्रलय के दिन उनके क्रियाकलाप को उचित-अनुचित ठहराया जाना उनके यहां भी स्वीकारा गया है। इन सभी स्थितियों में मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहने की बात को माना गया है।
अतीन्द्रिय विज्ञान भी क्रमशः इसी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है कि कुछ समय पूर्व भौतिक—विज्ञानवेत्ता शरीर से प्रथक कोई स्वतन्त्र आत्मा न होने की जिस बात को जोरों के साथ कहते हैं, अब वह बात कुछ दमदार नहीं रही। पूर्वजन्मों की स्मृतियों वाले बालक उन ईसाई और मुसलमान—परिवारों में भी पाये गये हैं, जिनकी परम्परा पूर्वजन्म स्वीकार न करने की ही रही है। कितने ही बालक संगीत आदि की ऐसी अद्भुत प्रतिभा अतिन्यून आयु में ही प्रदर्शित करते हैं, जिसका मानव मस्तिष्क-विकास के स्वाभाविक—विकास के साथ कोई ताल-मेल नहीं खाता। इन अद्भुत उदाहरणों का समाधान ‘‘पूर्व जन्मों की विद्या का अनायास प्रकटीकरण’’ मानने के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं होता।
भूत-प्रेतों के अस्तित्व को विज्ञ-समाज में अन्ध विश्वास और वहम भर माना जाता रहा है। पर कठोर अन्वेषण की परीक्षा—कसौटी पर खरे उतरने वाले प्रमाण सामने आये हैं, जिनमें भूतात्माओं के अस्तित्व से इन्कार करने की गुंजाइश नहीं रहती। प्रचलित भूतवाद के ढकोसलों में बहुत कुछ ‘वहम’ हो सकता है, पर यत्र-तत्र ऐसे भी प्रमाण सामने आते हैं—जिन्हें देखते हुए मरण के उपरान्त भी आत्माओं के किसी रूप में बने रहने और हलचलें करने की बात को स्वीकार करना ही पड़ता है।
नव-जात शिशुओं में माता का दूध पीने का स्थान ढूंढ़ निकालना आदि कितनी ही ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिन्हें देखते हुए यही मानना पड़ता है कि पूर्वसंचित ज्ञान के बिना यह सब अनायास ही नहीं हो सकता। अनुवांशिकी-विज्ञान में पैतृक ज्ञान के फलित होने का प्रतिपादन अवश्य है, पर वह भी यहां आश्चर्य चकित है कि बिना प्रशिक्षण या बिना आधार के जीव धारियों के बालक कैसे जीवनोपयोगी रीति-नीति ही विकसित कर लेते हैं? पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते रहने वाले पक्षी किस प्रकार मार्ग की दुर्लभ्य कठिनाइयों को नपे-तुले ढंग से पार करते हैं और कुछ विशेष प्रकार की ईल जैसी मछलियां कैसे सहस्रों मील की यात्रा करने प्रणय-प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान पर जाती और फिर वर्षों में पूरी होने वाली उस लम्बी यात्रा को पूरी करके यथा स्थान वापिस लौटती हैं? प्राणियों के सहज ज्ञान की श्रृंखला इतनी विलक्षण है कि वंशानुक्रम की सम्भावनाएं उसका समाधान कर नहीं पातीं। कीव-विज्ञानी अब यह सोचने लगे हैं कि इस संचित ज्ञान का आधार जीवधारियों के पुनर्जन्म से सम्बन्धित होना चाहिए।
जो हो, किसी न किसी आधार पर प्रायः हर वर्ग का व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मृत्यु के बाद ही जीवन का अन्त नहीं हो जाता, वरन् पीछे भी बना रहता है। शरीर के बिना भी जो जीवित रहता है, उसे आत्मा ही कहा जायगा। इस प्रकार यह मरणोत्तर जीवन की मान्यता आस्तिकों तक ही सीमित नहीं रही, वरन् नास्तिक वर्ग भौतिक प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य को क्रमशः स्वीकार करता चला जा रहा है।
प्रश्न यह है कि जब शरीर से प्रथम आत्मा के अस्तित्व की जानकारी प्रायः सभी को है और हलके-भारी मन से उस तथ्य को किसी न किसी रूप में स्वीकार हो जाना है तो हमारा यह प्रयास क्यों नहीं होता कि आत्मा के ऐसे स्वार्थों की ओर भी ध्यान दिया जाय, तो शरीर से ही जुड़े हुए नहीं हो सकते। शरीर-सुख में इन्द्रिय-जन्य वासनाओं की तृप्ति ही मुख्य है। मन की मांग अदंता के पोषण करने वाली वस्तुओं तथा परिस्थितियों को जुटाने की रहती है। मोटे रूप से वासना और तृष्णा ही शरीर-सुख के दो आधार पाये जाते हैं। किन्तु देखा जाता है कि जिनके पास यह साधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं उनका भी अन्तःकरण इन उपलब्धियों से सन्तुष्ट नहीं होता, वरन् बहुत कुछ मिलने पर भी अशान्त, अतृप्त और उद्विग्न ही बना रहता है। अन्तरंग के मर्मस्थल में यह असन्तुष्ट सत्ता कौन है? निस्सन्देह इसे आत्मा ही कहा जायगा।
शरीर की मांग—भूख, वासना और तृष्णा के साधन जुटने पर तृप्त होनी चाहिए। होती भी है। भरपेट स्वादिष्ट आहार मिल जाने पर फिर उसकी अधिक मात्रा खाते नहीं बनती। काम-सेवन आदि की भी एक स्वल्प सीमा है। तृप्ति के बाद उस सन्दर्भ में भी जी ऊब जाता है, यही बात अन्य सब इन्द्रियों के बारे में भी है। तृप्ति के साधन जुट जाने के बाद भी जो घोर अतृप्त पाया जाता है, वह अन्तरात्मा ही है। उसकी आकांक्षाएं शरीर से भिन्न हैं। जब तक उन्हें पूरा करने के साधन न जुटें, तब तक उसका असन्तुष्ट रहना स्वाभाविक भी है। शरीर और आत्मा की भिन्नता और उनके पारस्परिक सम्बन्धों, स्वार्थों को समझने का नाम ही अध्यात्म है। जब तक वह भिन्नता समझी-स्वीकारी न जाय, तब तक मात्र शरीर का पोषण करने वाले प्रयास ही होते रहते हैं। आत्मा की स्थिति और आवश्यक समझे बिना उसके लिए कुछ सोचा किया भी कैसे जाय? इस एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह ही कहना चाहिए कि हम अपने आपको भूल बैठे हैं। अपने आपको अर्थात् आत्मा को। शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा अप्रत्यक्ष। चमड़े से बनी आंखें और मज्जा-तन्तुओं से बना मस्तिष्क केवल अपने स्तर के शरीर और मन को ही देख-समझ पाता है। जब तक चेतना-स्तर इतने तक ही सीमित रहेगा, तब तक शरीर और मन की सुख सुविधाओं की बात ही सोची जाती रहेगी। उससे आगे बढ़कर इस तथ्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकना सम्भव ही न होगा कि हमारी—आत्मा का—स्वरूप एवं लक्ष्य क्या है और आन्तरिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जा सकता है?
चिरस्थायी और गहन अन्तराल की तृप्ति को शान्ति कहते हैं और शरीर, मन की आकांक्षा पूर्ति कहलाती है। लोग सुख के लिए उछल-कूद करते रहते हैं, किन्तु शान्ति के सम्बन्ध में सोचते भी नहीं। फिर वह मिले कैसे? अशान्त अन्तःकरण की जलन-सुख साधनों की कुछ बूंदों से शान्त नहीं हो सकती। यही कारण है की धनाधीश, सत्ताधारी और सम्मानित व्यक्ति आन्तरिक दृष्टि से विक्षुब्ध ही बने रहते हैं। सूक्ष्म तत्वों को देखने—समझने के लिए एक विशेष दिव्य—दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, अध्यात्म की भाषा में उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। गायत्री—मन्त्र में इसी दिव्य प्रकाश को सविता का भर्ग मानकर उपास्य ठहराया गया है। यह दिव्य-दृष्टि जगे तो शरीर और मन्त्र के घेरे से ऊंचे उठकर वस्तु स्थिति को देखना—समझना सम्भव हो सकता है।
मोटी दृष्टि हमें शरीर और मन की परिधि तक ही सीमित रखती है। स्थूल पदार्थों के चिन्तन तक ही उसकी पहुंच है। आत्म-कल्याण की बात उस दृष्टि से सोची जाय तो पंच-तत्वों से बने धर्मोपकरणों का, तीर्थ—मन्दिर दान, उपवास जैसे साधनों का ही उपयोग करने की ही बात सूझती है।
आत्म-शान्ति का स्वरूप क्या हो सकता है? उसकी कल्पना स्वर्ग में आहार निवास उपभोग के प्रचुर साधनों की परिधि तक ही कल्पना करती है। मानो मरने के उपरान्त भी आत्मा वर्तमान शरीर को ही धारण किये रहेगी और उन्हीं प्रसाधनों के उपभोग से काम चलेगा। यह बात सूझती ही नहीं कि जब वासना-तृष्णा की साधन-सामग्री इस लोक में तृप्ति न दे सकी तो तथाकथित स्वर्ग में बताई गई सुख-सामग्री से आत्मा का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? इस चिन्तन को बचपन ही कहना चाहिए कि आत्म-शान्ति की आन्तरिक तृप्ति के सन्दर्भ में भी वासना-तृष्णा के साधना जुटाने वाले तथाकथित स्वर्गीय परिस्थितियों में ही आनन्द और सन्तोष मिलने की बात सोचें।
आत्मा एक दिव्य चेतना स्फुलिंग है—जिसे भावनात्मक उल्लास से साधनों में ही तृप्ति मिल सकती है। सद्भावनाओं से प्रेरित सत्प्रवृत्तियों में ही आत्मा की शान्ति का उद्गम केन्द्र है। उत्कृष्ट स्तर का चिन्तन जब कार्यरूप में परिणित होता है। तब वह परिस्थिति बनती है, जिसमें आत्मा को शान्ति एवं तृप्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार के आनन्द की आरम्भिक झांकी स्वाध्याय और सत्संग में मिल सकती है, जो काय-कलेवर और आत्मा की मित्रता का—उनके पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन विश्लेषण कर सके एवं वासना-तृष्णा की सुख-लिप्सा से ऊंचे उठकर उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता अपना-कर आन्तरिक उल्लास की उपलब्धि का मार्ग-दर्शन कर सके। विषय-चर्चा से जिस प्रकार कानों को रस मिलता है, मनोरम दृश्य देखकर आंखें जिस प्रकार मुदित होती है, उसी प्रकार आत्म-चेतना को उस उद्बोधन में प्रसन्नता मिलती है, जिसके आधार पर अन्तःकरण को सद्भावनाओं से ओत-प्रोत बनाया जा सके। आत्म-शान्ति का द्वार तब खुलता है, जब सत्प्रवृत्तियों से भरी-पूरी गतिविधियां अपना कर यह अनुभव किया जाता है कि जीवन के स्वरूप और लक्ष्य के अनुरूप गतिविधियां अपना कर अपूर्णता से पूर्णता की ओर कदम बढ़ते चल रहे हैं। उच्च भावनाओं के अनुरूप क्रियाकलाप जब बन पड़ता है तो जीवन-क्रम का वह स्वरूप बन जाता है, जिसमें आत्मा को शान्ति और तृप्ति प्राप्त हो सके, वह भव-बन्धनों से मुक्त होकर नर से नारायण बन सके। शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानना उत्तम है, पर पर्याप्त नहीं। उस ज्ञान का लाभ तब है, जब काय-कलेवर के उचित, आवश्यक स्वार्थों तक ही सीमित रहा जाय और अपनी शेष शक्ति को आत्मिक—शान्ति की, आत्मिक—तृप्ति की, आत्मिक-प्रगति की दिशा में नियोजित किया जाय। कहना न होगा कि यह प्रयोजन उत्कृष्ट—चिन्तन ओर आदर्श कर्तृत्व अपनाने से ही पूरा हो सकता है। जब आत्मा और शरीर की भिन्नता को—उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को समझ ही नहीं लिया जाता, वरन् शरीर की तुलना में आत्मा के महत्व को स्वीकार करते हुए आत्म-कल्याण के प्रयास में तत्पर हुआ जाता है, तब यह माना जाता है कि आत्म-ज्ञान की दिव्य किरणें अन्तःकरण में झांकने लगीं और आत्मा का स्वरूप जाना ही नहीं गया, वरन् उसका लक्ष्य भी माना गया।
आत्मा-परमात्मा की चर्चा वाग् विलास के लिए आये दिन होती रहती है। उसकी सार्थकता तभी है, जब शरीर गत स्वार्थों को सीमित करके आत्म-कल्याण के लिए आवश्यक रीति-नीति अपनाने की आकुलता उभरने लगे।
आत्मा ही विद्या है—
एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया—आचार्य प्रवर विद्या और अविद्या में भेद क्या है? श्वेताश्वतरोपनिषद का आचार्य उत्तर देता है— ‘‘क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या ।’’
हे तात! नाशवान् जड़ पदार्थ हैं वही अविद्या है तथा अविनाशी आत्मा ही विद्या रूप है। सूक्ष्म शरीर—
इसी उपनिषद् में अविनाशी आत्मा की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि—
अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्ध गुणेनात्मगुणेन चैव । आराग्र मात्रो ह्यपरौऽपि दृष्टः ।। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स तिज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पत ।। —श्वेता श्वतरोपनिषद् 5।8-9
अर्थात्—हे तात! वह अंगूठे जितना लघु होकर भी संकल्प-विकल्प युक्त (अर्थात् सोचता विचारता है तथा अपनी बुद्धि के गुण से और श्रेष्ठ कर्मों के गुण से सुई के अग्रभाग जैसे आकार वाला हो गया है ऐसा सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा भी ज्ञानियों ने देखा दे देखा है। बाल के सौवें अंश से भी सौवें अंश परिमाण वाला भाग ही प्राणी का स्वरूप जानना चाहिये वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिमाण वाला आत्मा असीम गुणों वाला हो जाता है।
इन दो ऋचाओं में शास्त्रकार ने जीवन के विराट-दर्शन को सूत्र-रूप में पिरो दिया है। प्रकट है कि शरीर दो प्रकार के परमाणुओं से बनता है एक होते हैं जड़ दूसरे चेतन। जड़ परमाणु चूंकि स्थूल हैं इसलिये वह दिखाई देते हैं किन्तु चेतना एक प्रकार की तरंग, शक्ति और प्रकाश रूप है और देह में इस प्रकार सोखी हुई है जिस प्रकार सूखी मिट्टी का ढेला जल की जज्ब (सोख लेता है कर लेता है। उसके अस्तित्व का प्रमाण बुद्धि है उसी के न रहने पर शरीर सोचने विचारने की क्रियायें बन्द कर देता है। इस शक्ति का सांसारिक प्रयोजनों में खर्च करते रहने से वह नष्ट होती रहती है और जीव छोटा से छोटा (शरीर से भी और योनियों से भी, होता चला जाता है अनेक कल्पित रूपों में वह अनेक शरीरों में तब तक भ्रमण करता रहता है जब तक श्रेष्ठ कर्मों के गुण से वह फिर से शक्ति संचय करता हुआ सूर्य के समान असीम और तेजस्वी नहीं हो जाता। यह भी कहा है कि ज्ञानियों ने उसे देखा है—ज्ञानियों! संबोधन का अर्थ ही है ज्ञान अर्थात् वह ज्ञान से ही देखा जा सकता है। ज्ञान कोई पदार्थ नहीं है वह निरपेक्ष अवस्था है अर्थात् जिस समय पदार्थ, समय, गति और कारण सभी एकाकार हो जाते हैं ध्यान की उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। ध्यान द्वारा ही वह आत्मा अपने प्रकाश रूप में दिखाई देता है।
आज का विज्ञान यों आत्मा के अस्तित्व तक पहुंच गया है पर इसी ध्यान और अनुभूति (ज्ञान) के अभाव में वह इस तत्व को मानने को तैयार नहीं होता। मनुष्य शरीर जिन छोटी-छोटी प्रोटोप्लाज्मा की ईंटों से बना है वह दो भागों में विभक्त है— 1. नाभिक (न्यूक्लियस) 2. साइटोप्लाज्म के अन्तर्गत जल, कार्बन, नाइट्रोजन, आकाश आदि सभी पंच भौतिक ठोस द्रव तथा गैस अवस्था वाले पदार्थ पाये जाते हैं विभिन्न प्राणधारियों का यहां तक कि मनुष्य-मनुष्य के साइटोप्लाज्म में फर्क होता है। यह वंशानुगत आहार पद्धति और जलवायु आदि पर आधारित है और परिवर्तनशील भी है। आहार के नियमों तथा एक स्थान से दूरी जलवायु वाले स्थान में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे शरीरों के स्थूल भाग में अन्तर आ सकता है पर अभी तक चेतन की अर्थात् नाभिक की क्रियाओं पर विज्ञान कोई नियन्त्रण नहीं पा सका अलबत्ता वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि नाभिक में ही मनुष्य की सारी बौद्धिक चेतना काम करती है। उसमें न केवल अमर व अविनाशी गुण सूत्र विद्यमान हैं वरन् वह सूत्र सारे ब्रह्माण्ड को नाप सकने की क्षमता से परिपूर्ण हैं। सारे शरीर में यह चैतन्य तत्व एक शक्ति, एक तरंग की भांति विद्यमान है उसी के न रहने पर शरीर नहीं रहता। यह चेतना ही है जो मनुष्य शरीर से लेकर सृष्टि के स्थूल कणों तक में व्याप्त हो रही है। जहां तक चेतना का अंश प्राकृतिक परमाणुओं से शक्तिशाली होना है यहां तक तो जड़ और चेतन का अन्तर स्पष्ट प्रतीत होता रहता है पर एक अवस्था ऐसी आती है जब जड़ता चेतनता पर पूरी तरह घटाटोप हो जाती है वही अवस्था है जब चेतना पूर्ण रूप से जड़ गुणों वाली अर्थात् कंकड़-पत्थर जैसी स्थिति में चला जाता है। मुख्य रूप से सृष्टि की चेतना एक ही है पर वह गुणों के द्वारा क्रमशः जड़ होती चली गई है जो जितना जड़ हो गया वह उतना ही उपभोग्य हो गया पर जिसने अपनी चेतना का जितना अधिक विकास किया वही उतना उपभोक्ता होता चला जाता है।
विकास शास्त्रियों ने मनुष्य को अन्यान्य जीवों का विकसित रूप बताया है। कहा नहीं जा सकता यह सिद्धान्त कितना सच है। किन्तु उन्होंने एक शरीर से दूसरे शरीर में विकास की जो कड़ियां बैठाई हैं। वह दरअसल सराहनीय और परिश्रम का काम था। इसी सिद्धान्त से आज यह भी पुष्ट किया जा सकता है यह आत्मा ही जड़ व चेतन सर्वत्र गतिशील है पेड़, पौधों को जड़ और चेतन के बीच की नीचे की कड़ी कहा जा सकता है और जीवित-ग्रहों को उच्च कड़ी। यह प्रतिपादन ही जड़ता से असीम चेतनता के विकास का प्रमाण माना जा सकता है।
यह चेतना जड़ में भी जाती है इसका प्रमाण है वृक्ष, वृक्ष को शास्त्रों में जड़ व चेतन की सन्धि योनि माना गया है। यलोस्टोन नेशनल पार्क (अमरीका) में जहां उबलता पानी पृथ्वी से निकलता है वहां पर चारों ओर लाल रंग का किनारा बन गया है। बहुत दिनों तक यह लाल रंग वैज्ञानिकों को हैरान किये रहा। ऐसा किन्हीं जलाशयों के किनारे नहीं मिलता फिर इस लाल रंग का रहस्य क्या है यह जानने के लिये शोध प्रारम्भ हुई तब पता चला कि यह कोई न होकर जीवित पदार्थ है। इतनी तेज गर्मी में जहां कि मनुष्य का हाथ झुलस जाता है, जीवन का अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिये आश्चर्य की तबा थी। इस आश्चर्य में एक और भी आश्चर्य बाद में समझ में आया। वह यह था कि इस जीवित पदार्थ में जीवन और निर्जीवन दोनों के गुण विद्यमान यह है फायलस स्यनोफाइटावर्ग की एक ‘‘अलगी’’ है। सामान्यतः ‘‘अलगी’’ में नीला हरा-सारहीन द्रव्य (पिगमेंट) क्लोरोफिल के साथ रहता है, पर कुछ में लाल रंग का भी द्रव्य होता है।
फायलम यूग्लेनो फाइटा में भी पौधे व जन्तुओं दोनों के गुण पाये जाते हैं। इसमें ‘‘क्लोरोफ्लास्ट’’ (इसी में क्लोरोफिल नामक हरा द्रव्य होता है जो मुख्यतः वृक्षों का गुण है) रहता है, वह इसके पौधा होने का प्रमाण है। लेकिन जिस प्रकार पौधों के कोशों (सेल्स) में दीवार (सेलवाल) होती है, उस तरह की दीवार इनमें नहीं होती। वरन् इनके चारों ओर पहुंचा भोजन इन्जाइम्स के द्वारा पचाया जाता है। इन्जाइम्स ये स्वयं निकालते हैं। यह भोजन अन्धेरे में पचा सकते हैं इनकी वृद्धि भी एक कोश में होती है कोशीय भित्ति (सेलबाल) के स्थान पर इनमें लचीली कोशीय झिल्ली होती है वह ठोस भूमि पर संकुलित होती और फैलती है तो इस क्रिया द्वारा वह चल भी लेती है। इनमें ‘आई स्पॉट’ भी होता है जिससे यह विश्वास किया जाता है कि यह देखते भी हैं। इसके ही पास में एक छिद्रवाहिनी (वेक्यूल) होती है वह पानी व भोजन चूसने तथा निकालने का भी काम करती है वोक्यूल ज्यादातर एक कोशीय जन्तुओं में होता है। इनमें एक जीवधारी के पोषण (न्यूट्रिशन) ग्रहण पचाना (हालिजिक) तथा लैंगिक प्रजनन (सैक्सुअल रिप्रोडम्शन) गुण भी होते हैं। इन सभी उदाहरणों से यह विदित होता है कि जिसे वनस्पति घट माना जाता है। वह भी एक जीव की ही कोई अवस्था है। इस प्रकार धीरे-धीरे अपनी चेतनता के रहे-सहे अंश को छोड़ता हुआ एक दिन पूर्ण जड़ स्थिति में चला जाता है।
जीवात्मा के उच्च श्रेणी विकास का प्रमाण है जीवित ग्रहों में प्लाज्मा की उपस्थिति। पृथ्वी के सभी जीवधारियों के शरीर ठोस और द्रव पदार्थों से बने हैं इन्हीं की एक अवस्था गैस। एक पदार्थ का आयतन जितना सघन होगा वस्तु उतनी ही ठोस होगी पर जितना-जितना वह द्रव तथा गैस रूप में आती जायेगी उसका आयतन बढ़ता जायेगा। ठोस की शक्ति से गैस की शक्ति बड़ी होती है पर गुणों की दृष्टि से गैस में भी ठोस के गुण रहते हैं। वैज्ञानिक अब यह भी मानने लगे हैं कि जीवन केवल ठोस स्थिति में ही नहीं द्रव व गैस की अवस्था में भी रह सकता है। वैज्ञानिकों को वह प्रमाण मिले हैं कि जब पृथ्वी तप्त तवे के समान जल रही थी तब भी एक कोषीय जीव पृथ्वी पर उपलब्ध थे। और जब एक नई शक्ति ‘‘प्लाज्मा’’ के ज्ञान ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि यदि गैस स्थिति में जीवन रह सकता है तो प्लाज्मा में भी रह सकता है। प्लाज्मा ‘‘प्राण शक्ति’’ का वैज्ञानिक नाम है। इसे सूक्ष्म शरीर या प्रकाश शरीर कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार प्लाज्मा कोई विशिष्ट वस्तु न होकर ठोस-द्रव तथा गैस की तरह ही पदार्थ की चौथी-अवस्था है (हिन्दी डाइजेस्ट सन् 1962 अप्रैल अंग पेज 69, आकाश में चमकते हुए तारे प्लाज्मा ही हैं। यह प्लाज्मा एक प्रकार का ईंधन या आहार ही है। तारागण उसे किस प्रकार ग्रहण करके अपना जीवन धारण किये हुए हैं अभी तक वैज्ञानिक यह जानने में समर्थ नहीं हो पाये पर विशिष्ट तत्वों से प्लाज्मा का निर्माण करके उन्होंने यह सिद्ध अवश्य कर दिया है कि जिस प्रकार हमारे शरीरों में नाभिकीय द्रव्य की उपस्थिति से ही साइटोप्लाज्मा का निर्माण होता है उसी प्रकार सितारों में भी नाभिकीय गुण होने चाहिये यदि ऐसा है तो फिर उन्हें भी जीवधारी ही मानना चाहिये जैसा कि भारतीय आर्ष-ग्रन्थों में सूर्य को आत्मा चन्द्रमा पृथ्वी आदि को भी देवता कहा है।
प्लाज्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी अत्यन्त शक्तिशाली पदार्थ है। एक पौण्ड नाइट्रोजन का प्लाज्मा से एक इंजिन पूरे एक वर्ष तक चल सकता है। गैस को अत्यधिक गर्म करने से इलेक्ट्रान तीव्र गति करते हैं और एक परमाणु का इलेक्ट्रान हट कर अलग हो जाता है व अन्य परमाणु आयन बन जाता है। यह आयनी भूत गैस ही प्लाज्मा कहलाती है। आजकल विद्युत तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाई जाती है। पर प्लाज्मा के बारे में ज्ञान से वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि यह विज्ञान जब पूरी तरह विकसित हो जायेगा तो तारों के झंझट से मुक्ति मिल जायेगा तक केवल चुम्बकीय आकर्षण द्वारा कहीं भी शक्ति पैदा कर ली जा सकेगी।
प्लाज्मा एक प्रकार का प्रकाश और ताप युक्त प्राण ही है। मनुष्य शरीर से लेकर अन्य चेतन धारियों में वही शक्ति जीवन का आधार है। इसी शक्ति के पतन से मनुष्य लघुतम बनता है तो इसी के विकास से वह सूर्य जैसी महान् गुणों वाली चेतना में अपना विकास करके विराट बन जाता है। इसी का नाम विद्या है इस विद्या की प्राप्ति के लिये भारतीय आचार्यों ने अनेक साधनायें विकसित की हैं। प्लाज्मा की शक्ति से ही अनुमान किया जा सकता कि आत्म-शक्ति के सूक्ष्म या प्रकाशीय विकास द्वारा मनुष्य कितना समर्थ व शक्तिशाली बन सकता है। जबकि आज का विज्ञान केवल जड़ की व्याख्या और उसी को यांत्रिक नियंत्रण में लगा है यही अविद्या है। अविद्या को हटाकर विद्या की प्राप्ति कर सकें तो शास्त्रकार के कथन के अनुसार अंगुष्ठ मात्र प्राणी सूर्य जैसा विराट् बन सकता है।
वहां न वर्ण भेद है न लिंग भेद
आत्मा के पशु पक्षियों, वृक्ष वनस्पति में भी होने की बात पर कितने विवाद हैं कहा नहीं जा सकता। इसका एक ही कारण है कि कोई भी दर्शन आत्म-सत्ता का सर्व सफल हल प्रस्तुत नहीं कर सका। अनुभूत और प्रायोगिक दर्शन होने के कारण इस प्रश्न को ही भारतीय योग विज्ञान ही सुलझाता रहता है एक ही वस्तु का अनेक रूपों में रूपान्तर किसी समय में समझ में न आने वाली बात हो सकती है पर आज तो वैज्ञानिक पदार्थ के स्थूल, हवा, वायु भूत तथा प्लाज्मा अनेक स्वरूप जान गये हैं। अतएव रूपान्तर कोई सयस्दा नहीं रही। फिर भी आत्मा नर है या नारी यह प्रश्न अक्सर उठता रहता है। तात्विक दृष्टि से प्रश्न में कोई वजन न होने पर भी जिज्ञासा का समाधान आवश्यक समझा गया।
आत्मा का आस्तित्व
आत्मा न नर है न नारी। वह एक दिव्य सत्ता भर है। समयानुसार—आवश्यकतानुसार वह तरह-तरह के रंग-बिरंगे परिधान पहनती बदलती रहती है। इसी को लिंग व्यवस्था समझना चाहिए। सर्दी की ऋतु में गरम और भारी कपड़े पहनने की आवश्यकता अनुभव होती है और गर्मी में हलके वस्त्र पहनने या नंगे रहने की इच्छा होती है। नर-मादा रूपों दो आवरण दो ऋतुओं के लिए हैं। आत्मा की जब जैसी रुचि होती है तब वह वैसे वस्त्र पहन लेता है। कभी गरम भारी कभी ठंडे—झीने। कभी खट्टा स्वाद चखने की इच्छा होती है कभी मीठा।
दामा के जीवन का अपना आनन्द है और अपना स्तर उसे देखे समझे और अनुभव किये बिना आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सो जब स्नेह वात्सल्य, समर्पण सेवा की प्रवृत्तियां उभारने की शिक्षा लेनी होती है तो नारी के शरीर में प्रवेश करके उस तरह का अध्ययन, अनुभव, अभ्यास करना होता है और जब शौर्य, साहस, पुरुषार्थ श्रम की कठोरता का शिक्षण आवश्यक होता है तब उसे नर कलेवर पहनना पड़ता है।
मृदुलता और कठोरता के उभयपक्षीय समन्वय से जीवधारी की समग्र शिक्षा हो पाती है यदि वह एक ही योनि में पड़ा रहे तो उसके आधे ही गुणों का विकास हो पायेगा और उस अपूर्णता के रहते सर्वांगीण पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा। अस्तु भगवान ने यह व्यवस्था बना रखी है कि जीवधारी कभी मादा शरीर में रहा करे कभी नर में। यह परिवर्तन धूप-छांह जैसे उभयपक्षीय आनन्द की अनुभूति कराता है और जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित ही नहीं अभ्यस्त भी रखता है।
यह सोचना ठीक नहीं कि नर जन्म-जन्मांतरों तक नर ही रहेगा और नारी को नारी ही रहना पड़ेगा। अभ्यास और रुचि परिपक्व हो जाय तो एक ढर्रा भी कई जन्मों तक चलता रह सकता है, पर यदि तीव्र उत्सुकता उत्कंठा हो तो वह परिवर्तन अगले ही जन्म में हो सकता है। नर यदि नारी जैसी मनोभूमि और गतिविधियां अपना कर उस तरह की उत्कण्ठा तीव्र करे तो अगला जन्म उसे नारी के रूप में भी मिल सकता है इसी प्रकार नारी के लिए यह सर्वथा सम्भव है कि वह पुरुषोचित गतिविधियां और मनोवृत्तियां अपनाकर अगला परिवर्तन अपनी अभिलाषा के अनुरूप करले। यों प्रकृति के नियमानुसार बिना किसी प्रयत्न के भी यह परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर शास्त्री यह तथ्य भली प्रकार जान गये हैं कि हर जीवधारी में नर और नारी की उभयपक्षीय सत्ता बीज रूप में विद्यमान रहती है। उसका जो पहलू उभरा रहता है उसी को समर्थ एवं सक्रिय रहने का अवसर मिलता है—और दूसरा पक्ष प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। यदि उभार दूसरी दिशा में वह निकले तो सुप्त पक्ष जागृत हो सकता है और जागृत को सुषुप्ति में चला जाना पड़ता है।
सृष्टि में ऐसे अगणित जीवधारी विद्यमान हैं जिनमें नर और नारी के दोनों पक्ष समान रूप से सक्रिय होते हैं। वे एक ही जीवन में कभी नर और कभी मादा बनते रहते हैं। जब उनका जी आता है अपने संकल्पबल से नर बन जाते हैं और जब उमंग उठती है नारी स्वभाव ही नहीं बिना किसी कठिनाई के नारी अंगों का भी विकास अधूरा नहीं होता, वरन् इस सीमा तक प्रखर होता है कि सन्तानोत्पादन भी भली प्रकार से हो सके। आज का नर कल नारी बन कर अपने पेट में गर्भ धारण करेगा और परसों बच्चे जनेगा यह बात विचित्र लगती है, पर है सर्वथा सत्य कितने जीवों में यही प्रवृति है और वे एक ही जीवन में इस प्रकार के उभय-पक्षीय आनन्द की अनुभूतियां लेते रहते हैं। उनके जीवन समुद्र में कभी नर का ज्वार आता है तो कभी नारी का भाटा। प्रकृति ने उन्हें इच्छानुसार आवरण बदलने की जो सुविधा दी है वैसी ही यदि मनुष्यों को भी मिली होती तो वे भी इस प्रकार का आनन्द, लाभ करते। इतना ही नहीं नर और नारी के बीच असमानता की जो खाई बन गई है उसके बनने का कोई कारण न रहता। फिर न कोई छोटा समझा जाता न कोई बड़ा। किसी को किसी पर आधिपत्य जमाने की खुराफात भी न सूझती।
गोल्ड इस्मिट, रोश, हरीसन आदि प्राणि वेत्ताओं ने तितलियों की कलम एक दूसरे को लगा कर उनका लिंग परिवर्तन कृत्रिम रूप से सम्भव बना कर दिखाया है। विज्ञानी डबल्यू. हीरम्स ने मछलियों की कई जातियां उभयलिंगी पाई है और कुछ प्रयोगों में छोटे आपरेशन करके उन्हें परिवर्तित लिंग का बनाया है। पक्षियों में भी लिंग परिवर्तन के आपरेशन बड़ी मात्रा में सफल हुये हैं।
कुछ कीड़े होते हैं जो एक ही शरीर में बार-बार उभय लिंगी परिवर्तन करते रहते हैं। वे कभी नर बन जाते हैं कभी मादा। कीट विज्ञानी प्रो. ओरटन ने ऐसे जीवों की खोज की थी जो एक ही जन्म में कभी नर रहते हैं कभी नारी। ओइस्टर ऐसे जन्तुओं में अग्रणी हैं। वे मादा की तरह अण्डे देने के बाद ही नर बन जाते हैं। और उभयपक्षीय लिंग में रहने वाली विभिन्नताओं का आनन्द लूटते हैं। आस्ट्रिना गिवासा, स्लग लाइयेकस जाति के जलचर भी उभयलिंगी रसास्वादन का क्रम परिवर्तन करते रहते हैं लिमेष्ट्रिया पतंगा भी इसी स्तर का है वह कभी नारी होता है तो कभी नर।
आयस्टर वर्ग-जाति का ‘मोलस्क’ घोंघा अपने लिंग परिवर्तन करता रहता है। कभी वह मादा होता है तो कभी नर। 40 साल की पूरी आयु यदि वह जी सके तो प्रायः एक दर्जन बार वह अपना लिंग परिवर्तन करता है।
सृष्टि में ऐसे जीव-जन्तुओं की संख्या कम नहीं जो उभयलिंगी होते हैं। एक ही शरीर में शुक्र और डिम्ब उत्पन्न करने वाली ग्रन्थियां होती हैं। जब उनमें प्रौढ़ता आती है तो प्रजनन स्राव आप प्रवाहित होते हैं और रक्त संसार के सहारे उनको आत्मरति का आनन्द प्रजनन का लाभ मिल जाता है। ड्रोसोफिला मक्खी हैव्रो ब्रेकन ततैये, सिल्क व्रम मोथ, वैनस मोथ, जिप्सी मोथ, ओलोकेसपिस जैसे अनेक पतंगे उभयलिंगी होते हैं।
समझा जाता है कि नर और मादा का संयोग होना सन्तानोत्पादन के लिए आवश्यक है। पर यह मान्यता बड़े आकार वाले विकसित जीवों पर ही एक सीमा तक लागू होती है। छोटे जीवों में अगणित जातियां ऐसी हैं जिनमें प्रजनन के लिए साथी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने शरीर में रहने वाली उभय योनियां समयानुसार स्वयं ही संयोग बना लेती हैं और उस आत्मरति से ही प्रजनन का अध्याय पूरा हो जाता है।
प्रजनन क्रिया के लिए यौन संयोग के अतिरिक्त एक और भी तरीका है अपने विकसित स्वरूप को विघटित कर देना ‘‘यह क्रिया वनस्पति जगत में ही निरन्तर होती है। बीज गलकर अंकुर और पत्र पल्लवों के रूप में विकसित होता है और एक से अनेक बनने का क्रम अपना कर कालान्तर में वही पुष्ट पौधा बनकर कितने ही नये बीज हर साल उत्पन्न करता है। यह अमैथुनी प्रजनन क्रिया वनस्पति जगत का सर्व विदित परिपाटी है।
गन्ना, गुलाब आदि अगणित पौधे उनके टुकड़े करके गाढ़ देने पर अलग-अलग पौधे बन जाते हैं। वट गूलर जैसे वृक्षों की बड़ी डालियां भी नये पेड़ का रूप धारण करती हैं विकसित पुष्पों के पराग हवा में उड़ कर एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। मक्खियां और तितलियां भी उनका स्थानान्तर करती रहती हैं इस प्रकार पराग युगल परस्पर योग संयोग मिलाकर बिना रति क्रिया के अपनी वंश वृद्धि करते रहते हैं।
छोटे जीवों में भी वह गुण होता है कि वे अपने शरीर से अपने ही सरीखी नई संतति उत्पन्न कर सकें। यों दूसरी जाति की उत्पत्ति तो सहज ही हो जाती है। पेट में सड़ा अन्न मलकृमि बनकर विष्ठा के साथ निकलता है शरीर पर चिपका हुआ मैल जुए, चीलर बनता है, जीवित या मृत शरीर का सड़ा हुआ मांस आंख से देखे जा सकने वाले कीड़ों के रूप में अनायास ही बदल जाता है। सड़े हुए फल और तरकारियों में भी उसी रंग रूप के कीड़े रेंगते देखे जा सकते हैं। यह प्रजनन ही है। सड़न को रतिक्रिया तो नहीं कह सकते और न उससे सहधर्मी जीव उत्पन्न होता है फिर भी इसे जीव उत्पादन तो कह ही सकते हैं। कीचड़ और गन्दगी में मक्खी, मच्छरों और रेंगने वाले कृमियों का उत्पन्न होना इसी स्तर का प्रजनन है।
जिनकी गणना जीवधारियों में की जाती है ऐसे प्राणी भी अपने शरीर के ही टुकड़े बखेर कर अपनी जाति के नये प्राणी को जन्म देकर विधिवत वंश वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए उन्हें जाड़ा ढूंढ़ने या रति-क्रिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना शरीर ही इसके लिये पर्याप्त होता है और उसी से उभयपक्षीय मिलन संयोग से लेकर प्रजनन तक की सारी आवश्यकतायें सुचारु रूप में सम्पन्न होती रहती हैं। ‘अमीबा’ और ‘डायटम’ जीव इसी स्तर के हैं। उनमें जब प्रौढ़ता आती है तो अपनी ही शरीर को फुला कर उसका भाग अलग छिटका देते हैं और वह एक स्वतन्त्र प्राणी बनकर अपनी अलग वंश परम्परा का संचालन करता है।
जीवित कहे जाने वाले प्रत्येक जीवधारी या जीवाणु में मेटाबोलिज्य उपापच्य प्रजनन शक्ति होती है। सृष्टि में जीवधारियों का उत्पादन अभिवर्धन कैसे उत्पन्न हुआ इसका युक्ति संगत एक मात्र उत्तर यही हो सकता है कि आदि जीवाणुओं में अपने आपको विखण्डित करने सन्तानोत्पादन करने की सरलतम योग्यता विद्यमान थी। उसी के आधार पर जीवधारियों की संख्या बढ़ी और परिस्थितियों के अनुरूप उनने अपनी काया तथा चेतना का विकास परिष्कार किया। रतिक्रिया का प्रचलन तो बहुत बाद में—तब हुआ-जब प्राणधारी एक लिंगी न रह कर द्विलिंगी बन गये और उन नर-मादा की जननेन्द्रियां स्पष्ट उभरीं तथा गर्भ धारण के योग्य हो गई। इससे पूर्व अपने शरीर से विखण्डित होकर ही पीढ़ियां बढ़ाने का प्रचलन था। इसके आगे-मध्यकाल-में उभयलिंगी अन्तःस्राव मात्र उभय और पुष्प-पराग की तरह जीवधारी नर-मादा परस्पर स्नेह आलिंगन का क्रिया-कलाप गन्ध मादकता के आधार पर करने लगे थे। उतने से ही उनमें प्रजनन उपयोगी हलचलें उठ खड़ी होती थीं और सन्तान होने लगती थी यौन संसर्ग तो बहुत बाद की प्रगतिशीलता है।
सेलों के भीतर भरे न्यूक्लिक ऐसिड के माध्यम से पूर्वजों की शारीरिक, मानसिक विशेषतायें सन्तान में हस्तान्तरित होती है। एडमोसिन फास्टेट रसायन का होना प्रजनन योग्यता के लिए आवश्यक है। इन तत्वों को यदि प्राणियों में घटाया-बढ़ाया जा सके तो उनकी प्रजनन क्षमता का स्तर भी बदल सकता है। यह असम्भव नहीं कि क्षुद्र जीव अनभ्यस्त रतिक्रिया अपनाने लगे और सुविकसित प्राणी जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, अकेला—बिना सहचर के—बिना रति-क्रिया के सुयोग्य सन्तान का उत्पादन कर सकें।
पेप्टाइड रसायन का यह विदित गुण है कि गरम करने पर वह पानी में घुलता है और ठण्डा होने पर छोटे पिण्ड की शकल धारण कर लेता है। बाहर से उपयुक्त रासायनिक भोजन मिले और उपयुक्त ऊर्जा का वातावरण मिले तो उनमें विभाजन प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। इसी आधार पर जीवशास्त्री कृत्रिम जीवाणु उत्पन्न करने और उनसे वंश-वृद्धि का उपक्रम आरम्भ कराने के लिए प्रयत्नशील है।
आये दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिनमें नर के भीतर नारी के अथवा नारी के भीतर नर के यौन चिह्न विकसित होते चले गये और स्थिति यहां तक जा पहुंची की आपरेशन करके उनका लिंग परिवर्तन करना पड़ा। यह परिवर्तन इतना सफल रहा कि उन्होंने जोड़ा बनाया और सफल दाम्पत्य जीवन जीते हुए सन्तानोत्पत्ति भी की। मनोविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के आधार पर यह सिद्धान्त मान्यता प्राप्त है कि लिंग परिवर्तन के लिए मानवी प्रयत्न बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन तो इस जन्म में भी हो सकते हैं अन्यथा अगले जन्म में तो वह सम्भावना शत-प्रतिशत साकार हो सकती है। पुराणों में इस प्रकार के अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें व्यक्तियों ने अपने संकल्प बल एवं साधना उपक्रम के द्वारा लिंग परिवर्तन में सफलता प्राप्त की है इन दिनों भले ही वे उपचार विस्मृत विलुप्त हो गये हों—इससे क्या—तथ्य तो जहां के तहां ही रहेंगे। आत्मा के सुदृढ़ संकल्प और प्रयत्न यदि प्रखर होवें तो किसी भी आत्मा के लिए अपना वर्तमान लिंग बदल लेने की पूरी पूरी सम्भावना हो सकती है।
कभी कभी किन्हीं पुरुषों में नारी प्रकृति और नारियों में पुरुष प्रकृति पाई जाती है। उनके हाव-भाव स्वभाव एवं आचरण में इस प्रकार का अन्तर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसका एक मात्र कारण यह है कि पिछले दिनों उनकी मन्द इच्छा लिंग परिवर्तन की तो रही पर उनमें प्रौढ़ता प्रखरता नहीं आई। यदि उनका संकल्प बल और प्रयत्न बलशाली रहा होता तो उन्हें इस प्रकार के आधे अधूरे परिवर्तन का सामना न करना पड़ता। इतने पर भी उनका प्रवृत्ति परिवर्तन की दिशा में ही मन चलता रहे तो यह आशा की जा सकती है कि इस विराम के उपरान्त वे अपनी अभीष्ट मनोवांछा के अनुरूप लिंग परिवर्तन का लक्ष्य अगले जन्म तक पूरा कर लेंगे।
कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें पुरुष के शरीर से भी बच्चों का जन्म हुआ है। भले ही वे भ्रूण अविकसित रहे हों और भले ही वे जुड़वा भाई समझे जा सकते हों पर उत्पत्ति तो नर शरीर से हो ही गई। इन उदाहरणों से यह तो सिद्ध होता ही है कि मात्र नारी के शरीर में ही नहीं—नर कलेवर में भी वह क्षमता मौजूद है कि गर्भ धारण करने से लेकर गर्भपोषण तक कि क्रिया सम्पादन कर सके। अवसर मिले तो इस सम्भावना का अधिक विकास भी हो सकता है ओर नारी की तरह ही नर भी प्रजनन कर्म कर सकने में समर्थ हो सकते हैं।
फ्रांस के एक 17 वर्षीय लड़के जीन जक्यूस लोरेन्ट को छाती के दर्द की शिकायत थी। डाक्टरों ने फेफड़े का ट्यूमर पाया और उसका आपरेशन किया, डाक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने ट्यूमर के स्थान पर 3 पौण्ड 15 ओंस वजन का एक विकसित अंगों वाला बच्चा निकाला।
ब्रिटिश पैथोलोजिस्ट ऐसोशियेशन ने एक भ्रूण को लड़के का जुड़वा भाई बताया है जो गर्भ-काल में किसी प्रकार उसके शरीर में प्रवेश कर गया और वही बढ़ता पलता रहा।
इसी प्रकार की एक घटना बरेली (उ. प्र.) के जिला अस्पताल में हुई। बदायूं निवासी एक दो वर्ष के बालक का आपरेशन पेट का ट्यूमर समझ कर किया गया पेट खोलने पर उसमें एक विकसित भ्रूण पाया गया। जिसे अधिक अन्वेषण के लिए सुरक्षित रख लिया गया।
नर के शरीर से बच्चे की उत्पत्ति की अनेकों घटनायें बहुचर्चित हैं और उनके विवरण पत्र पत्रिकाओं में विस्तार पूर्वक छपे हैं। सन् 1956 में टोक्यो अस्पताल में एक किशोर लड़के के पेट का आपरेशन करके उसमें से 11 ओंस का अपरिपक्व बच्चा निकाला था। बच्चे की टांगें, बाल एवं शरीर के अन्य भाग स्पष्ट थे। उसी साल सन् 1956 में उत्तर वियतनाम के हनोई अस्पताल में एक पुरुष का आपरेशन करके बच्चा निकाला था जो जन्मते समय रोया भी था।
सन् 1954 में पाकिस्तान के बहाबलपुर नगर के विक्टोरिया अस्पताल में डाक्टरों ने एक पुरुष का पेट चीर कर उसमें बच्चा निकाला था।
इन तथ्यों पर गहराई से विचार किया जाय तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि नर और नारी के कलेवर करती और बदलती रहने पर भी आत्मा की स्थिति दोनों से ऊपर है अथवा उभयपक्षीय सम्भावनाओं से भरपूर है। जो आज नर है कल नारी बनना पड़ सकता है। इसी प्रकार नारी को नर की भूमिका सम्पादित करने का अवसर भी मिलता है। जब यह आवरण सामयिक है। तो नर और नारी के बीच ऐसी दीवारें क्यों की जायं जिनमें अधिकार और कर्तव्य की खाई खड़ी की जाय। किसी को छोटा, किसी को बड़ा माना जाय। दोनों को मिलजुल कर ऐसी समाज व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे बदलते रहने वाली लिंगीय परिस्थिति में किसी आत्मा को असुविधा अथवा अन्याय का अनुभव न करना पड़े।