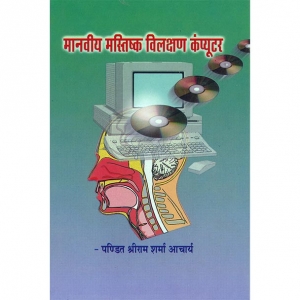मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्युटर 
मानसिक संतुलन यों साधें
Read Scan Version
सुख दुःख, प्रसन्नता खिन्नता, चिन्ता, भय और इसी तरह की अनुभूतियों जो मनुष्य को आनन्दित व प्रफुल्लित रखती हैं पूरी तरह मनः संस्थान से सम्बन्ध रखती है। एक पार्ट स्थिति किसी के लिए सुखद हो सकती है तो वही परिस्थिति किसी अन्य व्यक्ति के लिए अत्याधिक दुखद और कष्टकर हो सकती है। उसका कारण मानसिक स्थिति की बनावट ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सामान्य सी परेशानी के कारण भी इतना दुःखी उद्विग्न हो उठता है कि उसे अपना जीवन नाटकीय न जीने योग्य लगने लगता है। दूसरे कई व्यक्ति उससे भी कठिन और परेशानी उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के हंसते-हंसते झेल लेते हैं। इसका क्या कारण है? एक ही कारण कहा जा सकता है—मानसिक स्थिति की बनावट, संतुलित या असंतुलित मनःस्थिति।
जिन कारणों से मानसिक शांति नष्ट होती है, कार्य करने की क्षमता घटती है, परेशानी और उद्विग्नता बढ़ती है वे सभी कारण मस्तिष्कीय क्षमताओं को घटाते हैं साथ ही उन्हें रोगी और दुर्बल भी बनाते हैं। मस्तिष्कीय क्षमताओं का समुचित सदुपयोग करने के लिए आवश्यक है कि मानसिक संतुलन साधा जाये। ताकि सभी परिस्थितियों में शांत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हुए अभीष्ट दिशायें आगे बढ़ता रहा जा सके।
मानसिक संतुलन को साधने और सुस्थिर रखने का एकमेव उपाय है कि बाहरी प्रभावों से मुक्त रहते हुए अपने दृष्टिकोण और चिंतन की दिशा धारा को ऐसा मोड़ दिया जाये जिससे कि सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा जा सके। प्रत्येक परिस्थिति में मानसिक संतुलन स्थिर रखने के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। (1) प्रत्येक बुरी परिस्थिति से प्रभावित रहा जाय और (2) जिस किसी के भी सम्पर्क में आना पड़े उनके कारण अपने आपको विचलित न होने दें।
दृष्टिकोण बदलें
भली बुरी परिस्थितियों के कारण अधिकांश लोग प्रसन्न उद्विग्न होते हैं। उचित तो यह है कि दोनों परिस्थितियों में अपने आपको स्थिर रखा जाय। इतना न हो सके तो भी परिस्थितियों के बुरे प्रभाव से तो अपने को बचाना ही चाहिए। विपर्यय संसार का स्वाभाविक नियम है। दो विपरीत भावों को लाकर इसकी रचना की गई। रात-दिन, आलोक-अन्धकार, धूप-छांह, उदय-अस्त, जीवन-मरण, परिश्रम-विश्राम, निद्रा और जागरण एक अनादि, अविच्छिन्न क्रम का दूसरा नाम ही संसार है। जिस प्रकार संसार इस प्रतिभावात्मक क्रम के अन्तर्गत गतिशील है उसी प्रकार इसका परिणाम भी प्रतिभावात्मक ही है। सुख और दुःख संसार के केवल मात्र दो फल हैं। विविध रूपों और प्रकारों से प्रत्येक प्राणी इन फलों का स्वाद लेता हुआ जीवन-यापन कर रहा है।
यद्यपि सुख और दुःख संसार के दो फल हैं तथापि देखने में यही आता है कि अधिकतर लोग दुःखपूर्ण जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। हजारों में कदाचित् ही कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले, जो वास्तविक रूप में सुखी कहा जा सके। संसार में सुख होते हुए भी मनुष्य जो उससे वंचित दीखता है, उसका प्रमुख कारण उसकी अपनी मानसिक कमजोरी है। बाह्य परिस्थितियां मनुष्य को उतना परेशान नहीं करतीं जितना कि वह अपनी आन्तरिक दुर्बलता से दुःखी और व्यग्र होता है।
सुख-दुःख का अपना कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इनका उदय एक-दूसरे के अभाव में ही होता है और इन दोनों का उदय स्थल मनुष्य का मन है। जिस समय मन प्रसन्न और प्रफुल्ल होता है, संसार में चारों ओर सुख ही सुख दिखाई देता है। इसके विपरीत जब मन विषाद और निराशा से घिरा होता है तो हर दिशा में दुःख के ही दर्शन होते हैं। अस्तु, दुःख से बचने के लिये मन को सदा प्रसन्न, प्रफुल्ल उत्साह और आशापूर्ण बनाये रखना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभूति का मूल केन्द्र ‘मन’ जितना ही अधिक सबल और सशक्त होगा मनुष्य उतना ही सुखी और सन्तुष्ट रहेगा।
यदि अनुपात लगाकर देखा जाये तो ज्ञात होगा कि सुख की अपेक्षा मनुष्य दुःख ही अधिक भोग रहा है। इनका कारण यह नहीं है कि संसार में सुख की अपेक्षा दुःख अधिक है, बल्कि इसका कारण यह है कि मनुष्य ने अपनी दशा को दुःख के अनुकूल बना लिया है।
सांसारिक क्रम के अनुसार मनुष्य पर परेशानियों, कठिनाइयों और मुसीबतों का आना कोई अचम्भे की बात नहीं है। परेशान करने वाली परिस्थितियां सबके सम्मुख आती हैं और सभी को उनसे निपटना पड़ता है। अब यह एक भिन्न बात है कि कोई आई हुई विपत्ति पर विजय पा लेता है और उनसे दबकर कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहता है। आई हुई विपत्तियों को अपने पर हावी न होने देकर जो शान्त चित्त और स्थिर बुद्धि से उनके निराकरण का प्रयत्न करता है वह शीघ्र ही उन्हें दूर भगा देता है। किन्तु जो व्यक्ति किसी विपत्ति की संभावना अथवा उसके आने पर घबराकर अशान्त और उद्विग्न हो उठता है तो उसका सारा जीवन ही कटुतापूर्ण हो जाता है।
अशांत और उद्विग्न रहने वाले व्यक्ति के भाग्य से जीवन के सारे सुख उठ जाते हैं। उसके विकास और उन्नति की सारी सम्भावनायें नष्ट हो जाती हैं। निराशा और विषाद उसे रोग की तरह घेर लेते हैं। न उसे भोजन भाता है और न नींद आती है। जरा-जरा सी बात पर कुढ़ता, चिढ़ता और खीजता है। बड़ी-बड़ी अप्रिय एवं अस्वास्थ्यकर कुंठाओं से उसका हृदय भरा रहता है।
अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि मानसिक अशांति मनुष्य के स्नायु संस्थान पर अनुचित बोझ डालकर उसे निर्बल बना देता है, जिससे विश्राम करने की अवस्था में भी उसे आराम नहीं मिलता। चिन्तित एवं उद्विग्न चित्त व्यक्ति गहरी नींद न आने के कारण जब सोकर उठता है, तो ताजगी और स्फूर्ति के स्थान पर भारी थकान अनुभव करता है। घन्टों तक उसका शरीर उससे कब्जे में नहीं आता। आलस्य, शैथिल्य एवं निर्बलता आदि उसको बुरी तरह से दबाये रहते हैं। इस प्रकार कष्टपूर्ण दिन बिताने के कारण उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और आयु घट जाती है। मानसिक अशांति को मानव-जीवन का जीता-जागता नरक ही कहना चाहिये।
जिस प्रकार शरीर में ताप की अधिकता हो जाने से ‘ज्वर’ नामक रोग हो जाता है उसी प्रकार अधिक चिंतित और उद्विग्न रहने वाले व्यक्ति को अशांति और चिंता का मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। मानसिक अशांति का एक ऐसा आंतरिक आंदोलन है, जिसके उठने से मनुष्य के सारे विवेक, विचार एवं ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। उसकी बुद्धि असंतुलित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह अशान्ति के कारणों का निराकरण कर सकने में सर्वथा असमर्थ रहता है और यदि उद्विग्न अवस्था में कोई उल्टे-सीधे प्रयत्न करता भी है तो उसके परिणाम उल्टे ही निकलते हैं। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ जाना, विषाद से छूटकर निराश हो उठना, क्रोध से छूटकर शोक और शोक से छूटकर भय के वशीभूत हो जाने का एक क्रम-सा बन जाता है। मानसिक असन्तुलन एक प्रकार की विक्षिप्तता ही होती है, जिसमें फंसकर मनुष्य किसी योग्य नहीं रहता। हर समय दुःखी, चिन्तित और परेशान रहना उसके जीवन क्रम का एक विशिष्ट अंग बन जाता है।
कोई कठिनाई अथवा आपत्ति अपने में उतनी भयंकर नहीं होती जितना कि उसे उसकी मानसिक अशांति जटिल और दुरूह बना देती है। आपत्तियों से छूटने का उपाय चिन्ता, भय, निराशा, आशंका आदि की प्रतिगामी भावना नहीं है बल्कि साहस, धैर्य और उत्साह की वृत्तियां ही होती हैं।
मानसिक अशांति मनुष्य के शरीर में एक भयंकर उत्तेजना में रहने वाले व्यक्ति के रक्त में विष का प्रभाव हो जाता है, जो रक्त के क्षार को नष्ट करके गठिया, यक्ष्मा आदि भयंकर रोगों में प्रकट होता है।
मानसिक अशांति एक भयंकर आपत्ति है। मनुष्य को हर सम्भव उपाय से इससे बचते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। विपत्तियों से घबराने, भयभीत होने, उनसे भागने अथवा उन्हें लेकर चिन्तित होने से आज तक कोई व्यक्ति छुटकारा न पा सका है। बहुधा देखा जाता है कि जो जितना अधिक चिन्तित और अशांत रहता है, वह और अधिक विपत्ति में फंसता है। इसके विपरीत जो शांतचित्त सन्तुलित मन और स्थिर बुद्धि से उनका सामना करता है, परेशानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। विपत्ति आने पर मनुष्य अपनी जितनी शक्ति को उद्विग्न और अशांत रहकर नष्ट कर देता है, उसका एक अंश भी यदि वह शान्त चित्त रहकर कष्टों को दूर करने में व्यय करे तो शीघ्र ही मुक्त हो सकता है।
आपत्तियों के आने पर घबराना नहीं चाहिये बल्कि धैर्यपूर्वक उनको हटाने का उपाय करना चाहिये। अधिकतर लोग कठिनाइयों को पार करने का मार्ग निकालने के बजाय अपनी सारी क्षमताओं को व्यग्र और विकल होकर नष्ट कर देते हैं। किंकर्तव्यविमूढ़ बनकर ‘क्या करें’ ‘कहां जायें’ ‘कैसे बचें’ आदि विर्तकना करते हुए बैठे रहते हैं, जिससे आई हुई विपत्ति भी सौगुनी होकर उन्हें दबा लेती है।
जीवन में जो भी दुःख-सुख आये उसे धैर्यपूर्वक तटस्थ भाव से सहन करना चाहिए। क्या सुख और क्या दुःख दोनों को अपने ऊपर से ऐसे गुजर जाने देना चाहिये जैसे वे कोई राहगीर है, जिनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं।
मनुष्य की मानसिक शांति और बौद्धिक सन्तुलन दो ऐसी अमोघ शक्तियां हैं, जिनके बल पर विकट से विकट परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। विपत्तियां आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। किन्तु जो व्यक्ति इनका प्रभाव ग्रहण कर लेता है वह मानसिक अशांति के रूप में आजीवन बनाये रहता है और ऐसे मनुष्य के लिये प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल फल ही उत्पन्न करती हैं। इस तरह न केवल दुःख अपितु सुख की अवस्था में भी वह दुःखी रहता है।
जीवन को सुखी और सन्तुष्ट बनाये रखने के लिये मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में अपनी मानसिक शांति को भंग न होने दें, इसकी उपस्थिति में सुख और भाव में दुःख की वृद्धि होती है।
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा
परिस्थितियों के बाद मनुष्य की मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है सक्की समाज में रहते हुए मनुष्य को कितने ही तरह के व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता है। सम्पर्क में आने वाले लोग कई तरह की प्रकृति के होते हैं। इन भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों से सम्पर्क में आते समय अपने आपको अविचल, अप्रभावित रखने के लिये ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहे, जल में कमल के पत्ते के समान अछूता रहे वह सुख और शान्ति को प्राप्त कर सकता है।
समाज में रहते हुए भी अपने आस-पास के लोगों से अप्रभावित रहना बहुत कठिन है। इस स्थिति को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पर ऐसे नियम हैं जरूर जिन्हें अपनाकर बाहरी व्यक्तियों के व्यवहार से अछूता रहा जा सकता है। इसी व्यवहार का स्वर्णिम सूत्र लिखते हुए महर्षि पातंजलि ने अपने ग्रन्थ योगदर्शन में कहा है— मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणा सुखदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनात्पश्चित्त प्रसादनम् ।
—1।22
अर्थात्—सुखी दुःखी पुण्यात्मा और दुष्टात्मा लोगों के प्रति मैत्री, करुणा, प्रफुल्लता और उपेक्षा भाव रखने से चित्त को अखण्ड प्रसन्नता मिलती है। स्वामी विवेकानन्द ने इस सूत्र का अर्थ खोलते हुए लिखा है—‘‘मन को इस प्रकार के विभिन्न भावों को ग्रहण करने में असमर्थता के कारण हमारे दैनिक जीवन में अधिकांशतः गड़बड़ी एवं अशान्ति होती है। मान लो, किसी ने मेरे प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया तो मैं तुरन्त उसका प्रतिकार करने के लिये उद्यत हो जाता हूं और इस प्रकार बदला लेने की यह भावना दर्शा देती है कि हम चित्त को दबा रखने में असमर्थ हो रहे हैं। वह उस वस्तु की ओर तरंगाकार में प्रवाहित होता है और उस हम अपनी मन की शान्ति खो बैठते हैं। हमारे मन में घृणा अथवा दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है वह मन की शक्ति का क्षय मात्र है। दूसरी ओर यदि किसी अशुभ विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाय तो उससे शुभकारी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिये संचित रहती है।’’
चित्त का प्रधान गुण है प्रतिक्रिया करना। वह एक फोटो प्लेट की भांति है जिसमें भले-बुरे भावों की वैसी ही फोटो आती है। फोटोग्राफर अच्छी तरह जानते हैं कि किस कोण पर खड़ा होने से तस्वीर अच्छी आयेगी और किस कोण पर भद्दी फोटो आयेगी। इस कोण को समझने और वही से चित्र लेने के कारण वे कुरूप से कुरूप वस्तु का भी अच्छा और सुन्दर चित्र खींच लेते हैं। चित्त के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। उसे जिस कोण पर सामने रखा जायेगा वहां से वह उसी तरह की तस्वीर खींचेगा। फोटोग्राफर को तो तस्वीर खींचने के लिये फिर भी कैमरे का बटन दबाना पड़ता है। पर मन तो सामने आते ही तस्वीर खींच लेता है और चित्त पर अंकित कर देता है।
प्रतिक्रियाओं से रहित हो जाना उन्हीं के लिये सम्भव है जो चित्त क्षय की आध्यात्मिक भूमिका में पहुंच चुके हों। पर सामान्य व्यक्तियों के लिये अपने कैमरे को ठीक कोण पर रखना ही एकमात्र उपाय है जिससे बाहर की घटनाओं का चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तत्ववेत्ताओं का कहना है कि मनुष्य मूलतः रोग और द्वेष के द्वन्द्वों में जीता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां अनर्थकारी कही गयी हैं। जिसके प्रति हमें रोग हो, वह आयु पूरी कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है, तो राग भंग होने का अवसाद मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियां या घटनायें व्यक्ति को अप्रिय होती हैं। वह उनके सम्पर्क में नहीं रहना चाहता। इसलिये उनसे घृणा होती है और यह घृणा ही द्वेष बन जाती है। संयोगवश उनका सम्पर्क होता है तो भी दुःख मिलता है।
व्यवहार क्षेत्र में हम राग और द्वेष को व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी देख सकते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रिय होते हैं, कुछ के सान्निध्य में रहने पर आकर्षण होता है, कुछ को देखने का मन नहीं करता और कुछ से चित्त बुरी तरह क्षुब्ध हो उठता है। योग-दर्शनकार ने इन्हें ही सुखी, पुण्यात्मा, दुःखी और दुष्टा कहा है। छोटे-छोटे वर्गीकरण न किये जायं तो हमारे आस-पास यह चार तरह के व्यक्ति ही भरे पड़े हैं। एक वे होते हैं जो हमारी अपेक्षा अधिक साधन सम्पन्न, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और सुखी होते हैं। उनकी स्थिति हमसे अच्छी होने के कारण प्रिय तो लगती है, पर चूंकि वही स्थितियां हमारे साथ नहीं होती इसलिए उन व्यक्तियों से ईर्ष्या होती है।
ईर्ष्या दाहकारी मनोविकार है। इस मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं उत्कर्ष करने के स्थान पर अपनी मानसिक शान्ति को ही नष्ट-भ्रष्ट करता रहता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा तो यह हो कि उन व्यक्तियों को भी प्रेम किया जाय और प्रेरणा ग्रहण की जाय। पर ‘अहं’ कहता है कि उस स्थिति के पात्र हम हैं और उस पर हमारा ही अधिकार रहना चाहिये। प्रगति का नियम है कि जो परिश्रम करता है और पुरुषार्थी बनने के रास्ते पर चलता है वही तरक्की करता है। ईर्ष्या से कभी किसी की प्रगति नहीं हुई है और न ही चाहने पर किसी का पतन होता है। उल्टे ईर्ष्या स्वयं अपने लिए ही हानिकर बन जाती है। शास्त्रकारों ने उन्नति के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले इस विकार को दूर करने का उपाय बताया है—मैत्री। मैत्री का अर्थ है सद्भावना पूर्ण आत्मीयता। आत्मीयता के सम्बन्ध जिससे भी स्थापित किये जायं वह सहयोगी बन जाता है और सहयोग व्यक्ति के विकास में सहायक ही बनता है। देखा जाय तो दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े और ऊंचे उठे उन्होंने जितना स्वयं के उत्कर्ष हेतु प्रयत्न किया उतना ही प्रयत्न अपने से अच्छी स्थिति वालों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी किया।
प्रगति की मंजिल इतनी दूर है और साधन तथा समय इतने स्वल्प होते हैं कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। स्वयं के द्वारा ही यदि कोई व्यक्ति मोटर चलाना सीखना चाहे, किसी की मदद लेना पसन्द न करे तो उसे मोटर की रचना प्रक्रिया समझने से लेकर उन्हें ड्राइव करना सीखने तक इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तथा इतना समय लगाना पड़ेगा कि सारा जीवन ही लग सकता है। इससे हासिल कुछ नहीं होता। अगर होता भी है तो बड़ी मुश्किल से। इसलिए अनुभवी प्रशिक्षकों की मदद लेनी पड़ती है। अपने से अच्छी स्थिति वाले लोगों की मैत्री का अर्थ है उनसे सहयोग प्राप्त करने और उनके अनुभवों का लाभ उठाने का मार्ग तलाशना।
दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो कष्टकारी स्थिति में हैं, दुःखी हैं। गिरे हुए, अवनति में पड़े और पिछड़े लोगों का कष्ट देखकर मन में पीड़ा होती है। यह पीड़ा ही घनीभूत होकर घृणा में भी बदल जाती है। जो लोग दुःखी, दरिद्रों को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें दुःखीजनों से बैर है। इसका कुल कारण इतना ही है कि उनके मन में होने वाली पीड़ा घनीभूत हो कर घृणा में बदल गयी है। शरीर में लगे घावों को देखकर, उसकी सड़न, बदबू, पीव और मवाद देखकर भी आंखें फेर लेने को जी चाहता है। पर इसलिये तो लोग उस अंग को कष्ट नहीं देते। यह नाक, भौं सिकोड़ना तो इसी बात का प्रतीक है कि वह स्थिति सहन नहीं हो सकी है उसे देखने का साहस नहीं जुट पा रहा है।
शरीर के सड़े हुए घाव की चिकित्सा करना जिस तरह हम आवश्यक समझते हैं, उसी तरह वह भी आवश्यक है कि समाज में जहां कहीं भी कष्ट और पीड़ा दिखाई दें उसके निवारण का भी उपाय करें इसलिये शास्त्रकार ने दुःखीजनों के प्रति करुणा का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। शरीर के किसी अंग विशेष में पीड़ा होने पर हाथ, आंखें, मस्तिष्क और पांव जिस तरह उसे दूर करने में लग जाते हैं। उसी प्रकार दुःखी लोगों की सेवा सुश्रूषा में भी तत्परता बरतनी चाहिए। जुगुप्सा करने और नाक, भौं सिकोड़ने से तो हमारे चित्त में भी वह अवसाद निःसृत होकर आ जाता है। जबकि कष्ट निवारण के लिये किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप हार्दिक सन्तोष अनुभव होता है।
अपने आस-पास दृष्टि डालने पर ऐसे लोग भी दिखाई पड़ते हैं—जो प्रगति के लिये प्रबल प्रयत्न करने में जुटे हुए हैं। ऐसे भी हैं जो समाज के लिये अपनी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करने में प्रवृत्त हैं। उनके प्रयासों को सराहनीय मान कर प्रमुदित होना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना एक ऐसा गुण है जो अंधकार के वातावरण में भी आशा की ज्योति जलाता है। संसार में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। ईमानदार लोग भी हैं तथा बेईमान भी। इन दोनों तरह के लोगों में से किसी भी एक वर्ग पर ही दृष्टि गड़ाई जा सकती है और प्रफुल्लित होने के साथ-साथ खिन्न तथा निराश भी हुआ जा सकता है।
यह ठीक है कि दुनिया में बुरे तत्व भी हैं पर इनसे न निराश होने की आवश्यकता है और न ही भयभीत होने की। महर्षि पातंजलि ने दोनों तरह के लोगों के बीच निर्द्वन्द्व रहने तथा अच्छाई का सहयोगी बनने की प्रेरणा देते हुए कहा है—‘अच्छाइयों को देखकर प्रसन्न होओ, उन्हें प्रोत्साहन दो, व बुराइयों की उपेक्षा करो उन्हें निरुत्साहित करो। अच्छाइयों को देखकर प्रसन्न होने पर यह चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि दुनिया में बुराई बहुत बढ़ गयी है। अच्छे लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। ऐसे में किस प्रकार शांत रहा जाय।’’
जहां भी शुभ दृष्टि रखेंगे वहीं अच्छे तत्व जरूर मिल जायेंगे। बुरे लोगों में भी कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। उन्हीं का उपयोग कर लोग कुशल संगठन कर्त्ता बन कर महामानव तक बन जाते हैं और अशुभ दृष्टि से ही सब जगह देखा जाय तो न कहीं आशा बंधती दीखती है और न ही प्रकाश दिखाई देता है। अच्छाई जहां भी हो उसे उभार कर सुखप्रद परिस्थितियां निर्मित की जा सकती हैं। यदि बुराई को देख-देखकर ही चिंतित होते रहा जाय तो जी थोड़ी बहुत सम्भावना रहती है वह भी जाती रहती है। परिस्थितियों के प्रति परिष्कृत और यथार्थ पर दृष्टिकोण तथा समाज में सम्पर्क के प्रति मैत्री करुणा, मुदिता उपेक्षा की नीति अपनाने के जो भी परिणाम हों पर व्यक्तिगत रूप से अशुभ की। उपेक्षा और शुभ को ग्रहण करने की नीति अपना मानसिक संतुलन सुस्थिर ही रखती है। मानसिक संतुलन की यह स्थिरता मस्तिष्कीय क्षमताओं को न केवल उन्नत परिष्कृत करती है वरन् जीवन के सभी पक्ष पहलुओं को विकसित करती है। इस रीति नीति को अपना कर ही कोई व्यक्ति अपने आपको सही अर्थों में प्रफुल्लित, आनन्दित रह सकता है और सर्वतोमुखी प्रगति कर सकता है।
जिन कारणों से मानसिक शांति नष्ट होती है, कार्य करने की क्षमता घटती है, परेशानी और उद्विग्नता बढ़ती है वे सभी कारण मस्तिष्कीय क्षमताओं को घटाते हैं साथ ही उन्हें रोगी और दुर्बल भी बनाते हैं। मस्तिष्कीय क्षमताओं का समुचित सदुपयोग करने के लिए आवश्यक है कि मानसिक संतुलन साधा जाये। ताकि सभी परिस्थितियों में शांत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हुए अभीष्ट दिशायें आगे बढ़ता रहा जा सके।
मानसिक संतुलन को साधने और सुस्थिर रखने का एकमेव उपाय है कि बाहरी प्रभावों से मुक्त रहते हुए अपने दृष्टिकोण और चिंतन की दिशा धारा को ऐसा मोड़ दिया जाये जिससे कि सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा जा सके। प्रत्येक परिस्थिति में मानसिक संतुलन स्थिर रखने के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। (1) प्रत्येक बुरी परिस्थिति से प्रभावित रहा जाय और (2) जिस किसी के भी सम्पर्क में आना पड़े उनके कारण अपने आपको विचलित न होने दें।
दृष्टिकोण बदलें
भली बुरी परिस्थितियों के कारण अधिकांश लोग प्रसन्न उद्विग्न होते हैं। उचित तो यह है कि दोनों परिस्थितियों में अपने आपको स्थिर रखा जाय। इतना न हो सके तो भी परिस्थितियों के बुरे प्रभाव से तो अपने को बचाना ही चाहिए। विपर्यय संसार का स्वाभाविक नियम है। दो विपरीत भावों को लाकर इसकी रचना की गई। रात-दिन, आलोक-अन्धकार, धूप-छांह, उदय-अस्त, जीवन-मरण, परिश्रम-विश्राम, निद्रा और जागरण एक अनादि, अविच्छिन्न क्रम का दूसरा नाम ही संसार है। जिस प्रकार संसार इस प्रतिभावात्मक क्रम के अन्तर्गत गतिशील है उसी प्रकार इसका परिणाम भी प्रतिभावात्मक ही है। सुख और दुःख संसार के केवल मात्र दो फल हैं। विविध रूपों और प्रकारों से प्रत्येक प्राणी इन फलों का स्वाद लेता हुआ जीवन-यापन कर रहा है।
यद्यपि सुख और दुःख संसार के दो फल हैं तथापि देखने में यही आता है कि अधिकतर लोग दुःखपूर्ण जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। हजारों में कदाचित् ही कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले, जो वास्तविक रूप में सुखी कहा जा सके। संसार में सुख होते हुए भी मनुष्य जो उससे वंचित दीखता है, उसका प्रमुख कारण उसकी अपनी मानसिक कमजोरी है। बाह्य परिस्थितियां मनुष्य को उतना परेशान नहीं करतीं जितना कि वह अपनी आन्तरिक दुर्बलता से दुःखी और व्यग्र होता है।
सुख-दुःख का अपना कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इनका उदय एक-दूसरे के अभाव में ही होता है और इन दोनों का उदय स्थल मनुष्य का मन है। जिस समय मन प्रसन्न और प्रफुल्ल होता है, संसार में चारों ओर सुख ही सुख दिखाई देता है। इसके विपरीत जब मन विषाद और निराशा से घिरा होता है तो हर दिशा में दुःख के ही दर्शन होते हैं। अस्तु, दुःख से बचने के लिये मन को सदा प्रसन्न, प्रफुल्ल उत्साह और आशापूर्ण बनाये रखना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभूति का मूल केन्द्र ‘मन’ जितना ही अधिक सबल और सशक्त होगा मनुष्य उतना ही सुखी और सन्तुष्ट रहेगा।
यदि अनुपात लगाकर देखा जाये तो ज्ञात होगा कि सुख की अपेक्षा मनुष्य दुःख ही अधिक भोग रहा है। इनका कारण यह नहीं है कि संसार में सुख की अपेक्षा दुःख अधिक है, बल्कि इसका कारण यह है कि मनुष्य ने अपनी दशा को दुःख के अनुकूल बना लिया है।
सांसारिक क्रम के अनुसार मनुष्य पर परेशानियों, कठिनाइयों और मुसीबतों का आना कोई अचम्भे की बात नहीं है। परेशान करने वाली परिस्थितियां सबके सम्मुख आती हैं और सभी को उनसे निपटना पड़ता है। अब यह एक भिन्न बात है कि कोई आई हुई विपत्ति पर विजय पा लेता है और उनसे दबकर कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहता है। आई हुई विपत्तियों को अपने पर हावी न होने देकर जो शान्त चित्त और स्थिर बुद्धि से उनके निराकरण का प्रयत्न करता है वह शीघ्र ही उन्हें दूर भगा देता है। किन्तु जो व्यक्ति किसी विपत्ति की संभावना अथवा उसके आने पर घबराकर अशान्त और उद्विग्न हो उठता है तो उसका सारा जीवन ही कटुतापूर्ण हो जाता है।
अशांत और उद्विग्न रहने वाले व्यक्ति के भाग्य से जीवन के सारे सुख उठ जाते हैं। उसके विकास और उन्नति की सारी सम्भावनायें नष्ट हो जाती हैं। निराशा और विषाद उसे रोग की तरह घेर लेते हैं। न उसे भोजन भाता है और न नींद आती है। जरा-जरा सी बात पर कुढ़ता, चिढ़ता और खीजता है। बड़ी-बड़ी अप्रिय एवं अस्वास्थ्यकर कुंठाओं से उसका हृदय भरा रहता है।
अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि मानसिक अशांति मनुष्य के स्नायु संस्थान पर अनुचित बोझ डालकर उसे निर्बल बना देता है, जिससे विश्राम करने की अवस्था में भी उसे आराम नहीं मिलता। चिन्तित एवं उद्विग्न चित्त व्यक्ति गहरी नींद न आने के कारण जब सोकर उठता है, तो ताजगी और स्फूर्ति के स्थान पर भारी थकान अनुभव करता है। घन्टों तक उसका शरीर उससे कब्जे में नहीं आता। आलस्य, शैथिल्य एवं निर्बलता आदि उसको बुरी तरह से दबाये रहते हैं। इस प्रकार कष्टपूर्ण दिन बिताने के कारण उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और आयु घट जाती है। मानसिक अशांति को मानव-जीवन का जीता-जागता नरक ही कहना चाहिये।
जिस प्रकार शरीर में ताप की अधिकता हो जाने से ‘ज्वर’ नामक रोग हो जाता है उसी प्रकार अधिक चिंतित और उद्विग्न रहने वाले व्यक्ति को अशांति और चिंता का मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। मानसिक अशांति का एक ऐसा आंतरिक आंदोलन है, जिसके उठने से मनुष्य के सारे विवेक, विचार एवं ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। उसकी बुद्धि असंतुलित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह अशान्ति के कारणों का निराकरण कर सकने में सर्वथा असमर्थ रहता है और यदि उद्विग्न अवस्था में कोई उल्टे-सीधे प्रयत्न करता भी है तो उसके परिणाम उल्टे ही निकलते हैं। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ जाना, विषाद से छूटकर निराश हो उठना, क्रोध से छूटकर शोक और शोक से छूटकर भय के वशीभूत हो जाने का एक क्रम-सा बन जाता है। मानसिक असन्तुलन एक प्रकार की विक्षिप्तता ही होती है, जिसमें फंसकर मनुष्य किसी योग्य नहीं रहता। हर समय दुःखी, चिन्तित और परेशान रहना उसके जीवन क्रम का एक विशिष्ट अंग बन जाता है।
कोई कठिनाई अथवा आपत्ति अपने में उतनी भयंकर नहीं होती जितना कि उसे उसकी मानसिक अशांति जटिल और दुरूह बना देती है। आपत्तियों से छूटने का उपाय चिन्ता, भय, निराशा, आशंका आदि की प्रतिगामी भावना नहीं है बल्कि साहस, धैर्य और उत्साह की वृत्तियां ही होती हैं।
मानसिक अशांति मनुष्य के शरीर में एक भयंकर उत्तेजना में रहने वाले व्यक्ति के रक्त में विष का प्रभाव हो जाता है, जो रक्त के क्षार को नष्ट करके गठिया, यक्ष्मा आदि भयंकर रोगों में प्रकट होता है।
मानसिक अशांति एक भयंकर आपत्ति है। मनुष्य को हर सम्भव उपाय से इससे बचते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। विपत्तियों से घबराने, भयभीत होने, उनसे भागने अथवा उन्हें लेकर चिन्तित होने से आज तक कोई व्यक्ति छुटकारा न पा सका है। बहुधा देखा जाता है कि जो जितना अधिक चिन्तित और अशांत रहता है, वह और अधिक विपत्ति में फंसता है। इसके विपरीत जो शांतचित्त सन्तुलित मन और स्थिर बुद्धि से उनका सामना करता है, परेशानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। विपत्ति आने पर मनुष्य अपनी जितनी शक्ति को उद्विग्न और अशांत रहकर नष्ट कर देता है, उसका एक अंश भी यदि वह शान्त चित्त रहकर कष्टों को दूर करने में व्यय करे तो शीघ्र ही मुक्त हो सकता है।
आपत्तियों के आने पर घबराना नहीं चाहिये बल्कि धैर्यपूर्वक उनको हटाने का उपाय करना चाहिये। अधिकतर लोग कठिनाइयों को पार करने का मार्ग निकालने के बजाय अपनी सारी क्षमताओं को व्यग्र और विकल होकर नष्ट कर देते हैं। किंकर्तव्यविमूढ़ बनकर ‘क्या करें’ ‘कहां जायें’ ‘कैसे बचें’ आदि विर्तकना करते हुए बैठे रहते हैं, जिससे आई हुई विपत्ति भी सौगुनी होकर उन्हें दबा लेती है।
जीवन में जो भी दुःख-सुख आये उसे धैर्यपूर्वक तटस्थ भाव से सहन करना चाहिए। क्या सुख और क्या दुःख दोनों को अपने ऊपर से ऐसे गुजर जाने देना चाहिये जैसे वे कोई राहगीर है, जिनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं।
मनुष्य की मानसिक शांति और बौद्धिक सन्तुलन दो ऐसी अमोघ शक्तियां हैं, जिनके बल पर विकट से विकट परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। विपत्तियां आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। किन्तु जो व्यक्ति इनका प्रभाव ग्रहण कर लेता है वह मानसिक अशांति के रूप में आजीवन बनाये रहता है और ऐसे मनुष्य के लिये प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल फल ही उत्पन्न करती हैं। इस तरह न केवल दुःख अपितु सुख की अवस्था में भी वह दुःखी रहता है।
जीवन को सुखी और सन्तुष्ट बनाये रखने के लिये मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में अपनी मानसिक शांति को भंग न होने दें, इसकी उपस्थिति में सुख और भाव में दुःख की वृद्धि होती है।
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा
परिस्थितियों के बाद मनुष्य की मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है सक्की समाज में रहते हुए मनुष्य को कितने ही तरह के व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता है। सम्पर्क में आने वाले लोग कई तरह की प्रकृति के होते हैं। इन भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों से सम्पर्क में आते समय अपने आपको अविचल, अप्रभावित रखने के लिये ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहे, जल में कमल के पत्ते के समान अछूता रहे वह सुख और शान्ति को प्राप्त कर सकता है।
समाज में रहते हुए भी अपने आस-पास के लोगों से अप्रभावित रहना बहुत कठिन है। इस स्थिति को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पर ऐसे नियम हैं जरूर जिन्हें अपनाकर बाहरी व्यक्तियों के व्यवहार से अछूता रहा जा सकता है। इसी व्यवहार का स्वर्णिम सूत्र लिखते हुए महर्षि पातंजलि ने अपने ग्रन्थ योगदर्शन में कहा है— मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणा सुखदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनात्पश्चित्त प्रसादनम् ।
—1।22
अर्थात्—सुखी दुःखी पुण्यात्मा और दुष्टात्मा लोगों के प्रति मैत्री, करुणा, प्रफुल्लता और उपेक्षा भाव रखने से चित्त को अखण्ड प्रसन्नता मिलती है। स्वामी विवेकानन्द ने इस सूत्र का अर्थ खोलते हुए लिखा है—‘‘मन को इस प्रकार के विभिन्न भावों को ग्रहण करने में असमर्थता के कारण हमारे दैनिक जीवन में अधिकांशतः गड़बड़ी एवं अशान्ति होती है। मान लो, किसी ने मेरे प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया तो मैं तुरन्त उसका प्रतिकार करने के लिये उद्यत हो जाता हूं और इस प्रकार बदला लेने की यह भावना दर्शा देती है कि हम चित्त को दबा रखने में असमर्थ हो रहे हैं। वह उस वस्तु की ओर तरंगाकार में प्रवाहित होता है और उस हम अपनी मन की शान्ति खो बैठते हैं। हमारे मन में घृणा अथवा दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है वह मन की शक्ति का क्षय मात्र है। दूसरी ओर यदि किसी अशुभ विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाय तो उससे शुभकारी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिये संचित रहती है।’’
चित्त का प्रधान गुण है प्रतिक्रिया करना। वह एक फोटो प्लेट की भांति है जिसमें भले-बुरे भावों की वैसी ही फोटो आती है। फोटोग्राफर अच्छी तरह जानते हैं कि किस कोण पर खड़ा होने से तस्वीर अच्छी आयेगी और किस कोण पर भद्दी फोटो आयेगी। इस कोण को समझने और वही से चित्र लेने के कारण वे कुरूप से कुरूप वस्तु का भी अच्छा और सुन्दर चित्र खींच लेते हैं। चित्त के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। उसे जिस कोण पर सामने रखा जायेगा वहां से वह उसी तरह की तस्वीर खींचेगा। फोटोग्राफर को तो तस्वीर खींचने के लिये फिर भी कैमरे का बटन दबाना पड़ता है। पर मन तो सामने आते ही तस्वीर खींच लेता है और चित्त पर अंकित कर देता है।
प्रतिक्रियाओं से रहित हो जाना उन्हीं के लिये सम्भव है जो चित्त क्षय की आध्यात्मिक भूमिका में पहुंच चुके हों। पर सामान्य व्यक्तियों के लिये अपने कैमरे को ठीक कोण पर रखना ही एकमात्र उपाय है जिससे बाहर की घटनाओं का चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तत्ववेत्ताओं का कहना है कि मनुष्य मूलतः रोग और द्वेष के द्वन्द्वों में जीता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां अनर्थकारी कही गयी हैं। जिसके प्रति हमें रोग हो, वह आयु पूरी कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है, तो राग भंग होने का अवसाद मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियां या घटनायें व्यक्ति को अप्रिय होती हैं। वह उनके सम्पर्क में नहीं रहना चाहता। इसलिये उनसे घृणा होती है और यह घृणा ही द्वेष बन जाती है। संयोगवश उनका सम्पर्क होता है तो भी दुःख मिलता है।
व्यवहार क्षेत्र में हम राग और द्वेष को व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी देख सकते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रिय होते हैं, कुछ के सान्निध्य में रहने पर आकर्षण होता है, कुछ को देखने का मन नहीं करता और कुछ से चित्त बुरी तरह क्षुब्ध हो उठता है। योग-दर्शनकार ने इन्हें ही सुखी, पुण्यात्मा, दुःखी और दुष्टा कहा है। छोटे-छोटे वर्गीकरण न किये जायं तो हमारे आस-पास यह चार तरह के व्यक्ति ही भरे पड़े हैं। एक वे होते हैं जो हमारी अपेक्षा अधिक साधन सम्पन्न, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और सुखी होते हैं। उनकी स्थिति हमसे अच्छी होने के कारण प्रिय तो लगती है, पर चूंकि वही स्थितियां हमारे साथ नहीं होती इसलिए उन व्यक्तियों से ईर्ष्या होती है।
ईर्ष्या दाहकारी मनोविकार है। इस मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं उत्कर्ष करने के स्थान पर अपनी मानसिक शान्ति को ही नष्ट-भ्रष्ट करता रहता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा तो यह हो कि उन व्यक्तियों को भी प्रेम किया जाय और प्रेरणा ग्रहण की जाय। पर ‘अहं’ कहता है कि उस स्थिति के पात्र हम हैं और उस पर हमारा ही अधिकार रहना चाहिये। प्रगति का नियम है कि जो परिश्रम करता है और पुरुषार्थी बनने के रास्ते पर चलता है वही तरक्की करता है। ईर्ष्या से कभी किसी की प्रगति नहीं हुई है और न ही चाहने पर किसी का पतन होता है। उल्टे ईर्ष्या स्वयं अपने लिए ही हानिकर बन जाती है। शास्त्रकारों ने उन्नति के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले इस विकार को दूर करने का उपाय बताया है—मैत्री। मैत्री का अर्थ है सद्भावना पूर्ण आत्मीयता। आत्मीयता के सम्बन्ध जिससे भी स्थापित किये जायं वह सहयोगी बन जाता है और सहयोग व्यक्ति के विकास में सहायक ही बनता है। देखा जाय तो दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े और ऊंचे उठे उन्होंने जितना स्वयं के उत्कर्ष हेतु प्रयत्न किया उतना ही प्रयत्न अपने से अच्छी स्थिति वालों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी किया।
प्रगति की मंजिल इतनी दूर है और साधन तथा समय इतने स्वल्प होते हैं कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। स्वयं के द्वारा ही यदि कोई व्यक्ति मोटर चलाना सीखना चाहे, किसी की मदद लेना पसन्द न करे तो उसे मोटर की रचना प्रक्रिया समझने से लेकर उन्हें ड्राइव करना सीखने तक इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तथा इतना समय लगाना पड़ेगा कि सारा जीवन ही लग सकता है। इससे हासिल कुछ नहीं होता। अगर होता भी है तो बड़ी मुश्किल से। इसलिए अनुभवी प्रशिक्षकों की मदद लेनी पड़ती है। अपने से अच्छी स्थिति वाले लोगों की मैत्री का अर्थ है उनसे सहयोग प्राप्त करने और उनके अनुभवों का लाभ उठाने का मार्ग तलाशना।
दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो कष्टकारी स्थिति में हैं, दुःखी हैं। गिरे हुए, अवनति में पड़े और पिछड़े लोगों का कष्ट देखकर मन में पीड़ा होती है। यह पीड़ा ही घनीभूत होकर घृणा में भी बदल जाती है। जो लोग दुःखी, दरिद्रों को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें दुःखीजनों से बैर है। इसका कुल कारण इतना ही है कि उनके मन में होने वाली पीड़ा घनीभूत हो कर घृणा में बदल गयी है। शरीर में लगे घावों को देखकर, उसकी सड़न, बदबू, पीव और मवाद देखकर भी आंखें फेर लेने को जी चाहता है। पर इसलिये तो लोग उस अंग को कष्ट नहीं देते। यह नाक, भौं सिकोड़ना तो इसी बात का प्रतीक है कि वह स्थिति सहन नहीं हो सकी है उसे देखने का साहस नहीं जुट पा रहा है।
शरीर के सड़े हुए घाव की चिकित्सा करना जिस तरह हम आवश्यक समझते हैं, उसी तरह वह भी आवश्यक है कि समाज में जहां कहीं भी कष्ट और पीड़ा दिखाई दें उसके निवारण का भी उपाय करें इसलिये शास्त्रकार ने दुःखीजनों के प्रति करुणा का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। शरीर के किसी अंग विशेष में पीड़ा होने पर हाथ, आंखें, मस्तिष्क और पांव जिस तरह उसे दूर करने में लग जाते हैं। उसी प्रकार दुःखी लोगों की सेवा सुश्रूषा में भी तत्परता बरतनी चाहिए। जुगुप्सा करने और नाक, भौं सिकोड़ने से तो हमारे चित्त में भी वह अवसाद निःसृत होकर आ जाता है। जबकि कष्ट निवारण के लिये किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप हार्दिक सन्तोष अनुभव होता है।
अपने आस-पास दृष्टि डालने पर ऐसे लोग भी दिखाई पड़ते हैं—जो प्रगति के लिये प्रबल प्रयत्न करने में जुटे हुए हैं। ऐसे भी हैं जो समाज के लिये अपनी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करने में प्रवृत्त हैं। उनके प्रयासों को सराहनीय मान कर प्रमुदित होना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना एक ऐसा गुण है जो अंधकार के वातावरण में भी आशा की ज्योति जलाता है। संसार में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। ईमानदार लोग भी हैं तथा बेईमान भी। इन दोनों तरह के लोगों में से किसी भी एक वर्ग पर ही दृष्टि गड़ाई जा सकती है और प्रफुल्लित होने के साथ-साथ खिन्न तथा निराश भी हुआ जा सकता है।
यह ठीक है कि दुनिया में बुरे तत्व भी हैं पर इनसे न निराश होने की आवश्यकता है और न ही भयभीत होने की। महर्षि पातंजलि ने दोनों तरह के लोगों के बीच निर्द्वन्द्व रहने तथा अच्छाई का सहयोगी बनने की प्रेरणा देते हुए कहा है—‘अच्छाइयों को देखकर प्रसन्न होओ, उन्हें प्रोत्साहन दो, व बुराइयों की उपेक्षा करो उन्हें निरुत्साहित करो। अच्छाइयों को देखकर प्रसन्न होने पर यह चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि दुनिया में बुराई बहुत बढ़ गयी है। अच्छे लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। ऐसे में किस प्रकार शांत रहा जाय।’’
जहां भी शुभ दृष्टि रखेंगे वहीं अच्छे तत्व जरूर मिल जायेंगे। बुरे लोगों में भी कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। उन्हीं का उपयोग कर लोग कुशल संगठन कर्त्ता बन कर महामानव तक बन जाते हैं और अशुभ दृष्टि से ही सब जगह देखा जाय तो न कहीं आशा बंधती दीखती है और न ही प्रकाश दिखाई देता है। अच्छाई जहां भी हो उसे उभार कर सुखप्रद परिस्थितियां निर्मित की जा सकती हैं। यदि बुराई को देख-देखकर ही चिंतित होते रहा जाय तो जी थोड़ी बहुत सम्भावना रहती है वह भी जाती रहती है। परिस्थितियों के प्रति परिष्कृत और यथार्थ पर दृष्टिकोण तथा समाज में सम्पर्क के प्रति मैत्री करुणा, मुदिता उपेक्षा की नीति अपनाने के जो भी परिणाम हों पर व्यक्तिगत रूप से अशुभ की। उपेक्षा और शुभ को ग्रहण करने की नीति अपना मानसिक संतुलन सुस्थिर ही रखती है। मानसिक संतुलन की यह स्थिरता मस्तिष्कीय क्षमताओं को न केवल उन्नत परिष्कृत करती है वरन् जीवन के सभी पक्ष पहलुओं को विकसित करती है। इस रीति नीति को अपना कर ही कोई व्यक्ति अपने आपको सही अर्थों में प्रफुल्लित, आनन्दित रह सकता है और सर्वतोमुखी प्रगति कर सकता है।