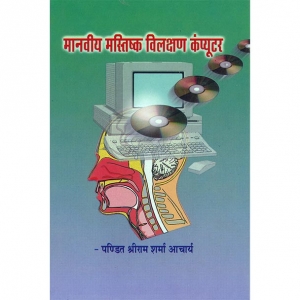मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्युटर 
न घुटते रहिये न भयभीत ही होइये
Read Scan Version
मस्तिष्क को—मानसिक शक्तियों के केन्द्र को आज व्यस्त और असंतुलित करने वाले कारणों में दो बहुत भयंकर हैं पहला घुटन और दूसरा भय। यों ये दोनों विकृतियां लगभग एक जैसी हैं। इनमें बहुत सूक्ष्म सा अन्तर है। घुटन में परिस्थितियों की प्रतिक्रिया होती है, उनसे होने वाली हानि के कारण घबड़ाहट भी होती है, परन्तु व्यक्ति उन परिस्थितियों के कारण इतना भयभीत रहता है कि वह भीतर ही भीतर घुलता जलता रहता है। भय में भी इसी प्रकार की दुर्बलता है। और ये दोनों स्थिति मानसिक असंतुलन के ही दुष्परिणाम हैं।
मस्तिष्क का पूरा नियन्त्रण सारे शरीर पर है, उसकी इच्छा से ही नाड़ी संस्थान काम करता है और ज्ञान तन्तुओं के माध्यम से ही उसी का वर्चस्व छोटे से लेकर बड़े अंगों पर छाया रहता है। ऐसे उद्गम केन्द्र में असन्तुलन पैदा होता हो तो वह स्थानीय नहीं हो सकता, उसका प्रभाव ज्ञान तन्तुओं के माध्यम से अन्य अंगों तक भी पहुंचेगा और वहां भी रुग्णता की संभावना उत्पन्न होगी।
मानसिक घुटन को वाणी द्वारा या क्रिया फूट कर बाहर निकलने का अवसर मिलना चाहिये। अन्यथा वह दबाव अनैच्छिक संस्थान की ओर मुड़ जाता है और शरीर में जो स्वसंचालित क्रियाएं होती रहती हैं उनमें वह घुटन वाला विष जा घुलता है। इससे सम्बन्धित अंगों में सिकुड़न एवं अकड़न पैदा होती है। यदि यह घुटन पेट की ओर मुड़ जाये तो आमाशय पर अकारण ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है और पाचन क्रिया में गड़बड़ मच जाती है। रक्त संचार रुकता है और पाचन रसों की सप्लाई रुक जाती है। उस गड़बड़ी से पहले आमाशय में सूजन होती है फिर जख्म बन जाते हैं। अल्सर इसी प्रकार का रोग है जिसमें शारीरिक कारण कम और मानसिक अधिक रहते हैं।
यदि शोक-सन्ताप का कोई कारण हो तो जोर से रो पड़ने का फूट-फूटकर बिलखने की इच्छा पूरी कर लेनी चाहिये मानसिक आघात से उत्पन्न घुटन बाहर निकाल देने का यही सरल और स्वाभाविक तरीका है। यदि लोक-लाज वश उस इच्छा को दबाकर अपने वीतराग या मनस्वी होने का ढोंग किया जायगा तो मानव स्वभाव की कमजोरियों पर तो विजय पाई न जा सकेगी, वह घुटन भी दबकर भीतर बैठ जायगी और अनेक गड़बड़ियां पैदा करेगी। कोई विषैली चीज पेट में पहुंच जाय तो सीधा तरीका यही है कि उल्टी या दस्त द्वारा बाहर निकल जाने दिया जाय यदि उसे निकलने का अवसर न मिला तो वह विष फिर अनेक भयंकर तरीकों से फूट कर निकलेगा। और दस्त उल्टी जैसी कठिनाई की तुलना में अधिक कष्ट साध्य और समय साध्य होगा।
क्रोध में बकझक कर, जी की जलन शान्त कर लेना अच्छा है। पर यदि उस आवेग को मन में दबा लिया जाय तो वह घृणा या द्वेष के रूप में जड़ जमा कर बैठ जायगा और शत्रुता का रूप धारण करके किसी अवसर पर विकराल प्रतिहिंसा का रूप धारण कर सकता है।
कामुक आकांक्षाओं को होली जैसे त्यौहार पर एक दो दिन उच्छृंखल नाच-कूदकर—गा बजाकर निकाल देते हैं और जी हलका कर लेते हैं इसके विपरीत मन में काम विकार घुमड़ते रहें और बाहर से ब्रह्मचारी बनकर बैठा रहा जाय तो भीतर ही भीतर वह घुटन दूसरे रूप में फूटती है और कई प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न करती है। अच्छा यही है कि मन को ऐसा प्रशिक्षित किया जाय कि उसमें सौम्य सज्जनता ही स्वाभाविक हो जाय और विकार विकृतियों के लिए गुंजाइश ही न रहे। पर यदि क्रोध, शोक आदि आवेग उठ रहे हों तो उन्हें प्रकट होकर बाहर निकल जाने देना चाहिये।
कोई तो ऐसा सच्चा एवं विश्वस्त मित्र होना ही चाहिये जिसके सामने पेट के छिपे हुए हर रहस्य और भेद को प्रकट कर दिया जाय सके। पिछले पापों को भी किसी ऐसे विश्वस्त से कह ही देना चाहिये जो उन्हें हर किसी से कहकर निंदा का वातावरण तो न बनाये पर स्वयं सहानुभूति पूर्वक सुनले। बदले में घृणा भी न करे। छिपी बात को कह सकने योग्य उसे विश्वस्त समझा जाय इसके लिये मित्र की उदारता और आत्मीयता को सराहे। ऐसे मित्रों का होना मनोविकारों की घुटन से पीछा छुड़ाने का अच्छा तरीका है। अपने किये हुए पाप का प्रायश्चित्य कर लेना तो सबसे ही उत्तम है। उससे घुटन द्वारा होने वाली भयंकर संभावनाओं की तुलना में कहीं कम कठिनाई उठाकर, न केवल मन हलका कर लिया जाता है, वरन् कितने ही शारीरिक और मानसिक रोगों की जड़ भी कट जाती हैं।
मनः संस्थान में उत्पन्न घुटन विकृतियां भावनात्मक रोग उत्पन्न करती हैं। उन रोगों के अलग से लक्षण नहीं होते वरन् वे शारीरिक रोगों में मिलकर ही फूटते हैं। शारीरिक रोग यदि काय गत हों तो मामूली दवा-दारू ही अच्छा कर देती है। पुराने समय में जब लोग सरल जीवन जिया करते थे, मन में प्रसन्नता, निष्कपटता और निर्द्वन्दता का सन्तुलन बनाये रहते थे तब आज जैसी मानसिक रोगों की बाढ़ न थी। उस जमाने में केवल काय कष्ट ही होता था अस्तु उनके उपचार में कोई कठिनाई नहीं होती थी। अब प्रत्यक्षतः तो शारीरिक रोग ही दीखते हैं पर उनके पीछे मानसिक रोगों की जटिल ग्रन्थियां उलझी होती हैं, जब तक वे न सुलझें, दवा क्या काम करें। मानसिक रोगों की दवाएं अभी निकली नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि चिकित्सकों को चक्कर में डाल रखने वाले और दवाओं को झुठलाते रहने वाले रोगों का बाहुल्य औषधि उपचार की परिधि से बाहर निकलने लगे तो उसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं है।
भावनाएं यदि निर्मल उदात्त और उच्चस्तरीय हों तो उनसे हर दृष्टि में लाभ ही लाभ है। अन्तःकरण मस्तिष्क और शरीर इन तीनों की ही पुष्टि होती है। परिस्थिति वश यदि शोक, क्रोध जैसे अवसर आ जायं और विवेक उनके समाधान में समर्थ न हो तो उसे स्वाभाविक रीति से प्रकट हो जाने देना चाहिए। जितना सम्भव हो उतना मर्यादाओं का पालन किया जाय, विवेक द्वारा बड़ी दीखने वाली बात को छोटी करके उपेक्षा में डाल दिया जाय पर यदि वैसा न बन पड़े तो उसके प्रकटीकरण में भी हर्ज नहीं है।
कामवासना के पीछे मूलवृत्ति हास्य, विनोद और क्रीड़ा कल्लोल की—कोमल भावनाओं की उत्तेजना का आनन्द लेने की होती है। उसे दूसरे रूप में प्रकट और परिणत किया जा सकता है। छोटे बालकों को खिलाने, दुलारने से भी सौन्दर्य वासना और निर्मल हास, विलास की आवश्यकता पूरी हो जाती है। संगीत साहित्य जैसी ललित कलाओं का निर्माण ही इस आधार पर हुआ है कि उनसे भावनात्मक नीरसता को सरसता में परिणत होने का अवसर मिले। नर-नारी में भी निष्पाप हास्य विनोद चलता रह सकता है। कुटुम्ब में बहिन, भाई, देवर, भौजाई, चाची, भतीजे जैसे कई रिश्ते नर-नारी के बीच रहते हैं। इनमें परस्पर विचार विनिमय, हास्य-परिहास, वार्तालाप चलता रहे तो नर-नारी की पूरक आकांक्षाएं पवित्र स्तर पर पूरी होती रह सकती हैं और कामेच्छा का उदात्तीकरण होने से उन्हें भावनात्मक तृप्ति मिलती रह सकती है। पति-पत्नी के बीच भी शरीरों को न्यूनतम मात्रा में ही गला कर—व्यंग विनोद, उपहास-परिहास की शालीन प्रक्रिया अपनाकर मनःक्षेत्र को उल्लास भरा जा सकता है और वासना जन्य घुटन का सहज निष्कासन होता रह सकता है। इस स्थिति में ब्रह्मचर्य पालन कठिन नहीं पड़ता वरन् सरल हो जाता है।
भावनाओं का अनियन्त्रित उभार ठीक शरीर में चढ़े हुए बुखार की तरह है। बुखार में पाचन तन्त्र लड़खड़ा जाता है। कोई अवयव उत्तेजित होकर, अधिक काम कर रहा होता है कोई एकदम शिथिल पड़ गया होता है। ऐसे असन्तुलन में रोगी को दाह, प्यास, बेचैनी, दर्द आदि कितने ही कष्ट अनुभव होते हैं। भावनात्मक उभार को एक मस्तिष्कीय बुखार कहना चाहिये। कई बार वह तीव्र होता है कई बार मन्द। क्रोध, शोक और बेकाबू होकर प्रकट होने वाले आवेग तीव्र बुखार है। चिन्ता, निराशा, कुढ़न, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियां मन्द ज्वर हैं। आकांक्षाओं को इतनी बढ़ा लेना कि वर्तमान परिस्थिति में कार्यान्वित फलीभूत न हो सकें तो भी उनसे अतृप्ति जन्य क्षोभ उत्पन्न होता है और मानसिक सन्तुलन बिगड़ता है। उन्नति के लिए प्रयत्न करना बात अलग है। और महत्वाकांक्षाओं का पहाड़ खड़ा करके हर घड़ी असन्तोष का अनुभव करना बिलकुल अलग बात है। कितने ही व्यक्ति उपलब्धियों के लिए व्यवस्थित प्रयास तो कम करते हैं, कामनाओं के रंग-बिरंगे स्वप्न देखते रहते हैं। शेखचिल्ली की तरह लम्बी-चौड़ी बातें सोचते रहना तो सरल है पर उन्हें फलीभूत बनाने के लिये योग्यता साधन और परिस्थिति तीनों का ही तालमेल रहना चाहिये। इसके बिना महत्वाकांक्षाएं—ऐषणाएं केवल मानसिक विक्षोभ ही दे सकती हैं इस प्रकार की उड़ानें उड़ते रहने वाले अन्ततः निराशा जन्य मानसिक रोगों के जाल जंजाल में जा फंसते हैं।
भावनात्मक विकृतियां शरीर के उपयोगी अंगों पर तथा जीवन संचार की क्रियाओं पर बुरा असर डालती हैं उनके सामान्य क्रम को लड़खड़ा देती हैं और वह अवरोध किसी न किसी शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होता है। पापी मनुष्य दूसरों की जितनी हानि करता है। उससे ज्यादा अपनी करता है। दुष्कर्म कर लेना अपने हाथ की बात है पर उसकी प्रतिक्रिया जो कर्त्ता के ऊपर होती है, और आत्म धिक्कार की आत्म-प्रताड़ना की, जो भीतर ही भीतर मार पड़ती है उसे रोकना किसी के वश में नहीं रहता। पाप पुण्य के भले-बुरे फल मिलने की यही तो स्वसंचालित प्रक्रिया है। पाप कर्म के बाद अन्तःकरण में अनायास ही पश्चाताप और धिक्कार की प्रतिक्रिया उठती है। उससे शरीर और मन का सन्तुलन बिगड़ता है। दोनों क्षेत्र रुग्ण होते हैं। उसके फलस्वरूप जन-सहयोग का अभाव, असम्मान मिलता है। और सन्तुलन बिगड़ा रहने से हाथ में लिये हुए काम असफल होते हैं। इस सबका मिला-जुला स्वरूप शारीरिक मानसिक कष्ट के रूप में आधि-व्याधि बनकर सामने आता है। कर्मफल भोग की यही मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इससे बचाव करने के लिये निष्पाप जीवन क्रम अपनाने की आवश्यकता है। जो पाप पिछले दिन बन पड़े हैं उनके प्रायश्चित के लिये किसी सूक्ष्मदर्शी आत्मविद्या विज्ञानी से परामर्श लेने की आवश्यकता है।
‘साइको सोमेटिक’ रोगों की बाढ़ इन दिनों बौद्धिक विकास के दुरुपयोग ने उत्पन्न की है। होना यह चाहिए कि यदि प्रबुद्धता के दुरुपयोग का खतरा हो वहां मानसिक विकास का प्रयास न किया जाय यदि वह अनुचित लगता है और मस्तिष्कीय विकास आवश्यक लगता है तो उसे सन्मार्गगामी बनाये जाने की समुचित तैयारी पहले से ही रखनी चाहिये। विकसित मस्तिष्क यदि दुष्प्रवृत्तियों से भरा रहा तो निश्चित रूप ले वह अभिशाप सिद्ध होगा और उसका दंड जटिल कष्ट साध्य, दुराग्रही साइकोसोमेटिक रोगों के रूप में भुगतना पड़ेगा। यह मानसिक रोग झक्कापन, सनक, आवेश, मतिभ्रम, अर्ध विक्षिप्तावस्था, पागलपन आदि के रूप में भी हो सकते हैं और अन्य शारीरिक अवयवों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं।
घुटन एक—न दीखने वाली—न समझ में आने वाली बीमारी है, पर इसका कुप्रभाव किसी भी भयंकर रोग से कम नहीं होता। अतृप्त और असंतुष्ट मनुष्य अपने आप ही अपने आप को खाता, खोता और खोखला करता रहता है। घुटन से बचा जाय। यदि अपनी भूल है—स्थिति का सही मूल्यांकन न करके काल्पनिक जाल-जंजाल बुन लिया गया है तो मकड़ी के जाले को तोड़कर यथार्थता के धरातल पर आना चाहिये और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर मन का बोझ हलका करना चाहिये। यदि अपनी मान्यता सही है और दबाव डालकर आत्मा की आवाज का हनन किया जा रहा है तो फिर ऐसे आधिपत्य से इनकार करके अपना स्वतन्त्र रास्ता बनाना चाहिये फिर चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। घुटन में दिन काटते हुए अन्तरात्मा को दिन-दिन दुर्बल बनाते जाने से तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही बल नष्ट होते हैं। इस प्रकार आत्महत्या की स्थिति से तो निकलना ही चाहिए भले ही उसमें कुछ बड़ा जोखिम उठाना पड़े। घुटन यदि आत्म प्रताड़ना की है तो उसे किसी विश्वस्त मित्र के आगे जी खोलकर कह ही देना चाहिये इस प्रकार वह धुंआ बाहर निकाल देने पर ही जी हलका हो सकता है।
उसी से डरें जिससे डरना चाहिए—
संकट भयंकर जब तक लगता है जब तक उसके साथ मुठभेड़ नहीं होती। जब उसके साथ गुंथ जाया जाता है और मानसिक सन्तुलन बिगड़ने नहीं दिया जाता तो प्रतीत होता है कि जितना सोचा गया था—उससे आधी चौथाई भी उसकी वास्तविक भयानकता नहीं थी। संकटों के साथ गुंथने का जैसे-जैसे अभ्यास होता जाता है, वैसे-वैसे वे स्वाभाविक दैनिक कार्यों की तरह सरल प्रतीत होने लगते हैं।
अपने लिये सांप और शेर बहुत भयंकर होते हैं पर बहुत से लोगों का धन्धा ही उन्हें पकड़ना मारना है। सपेरे रोज ही काले विषधर नाग पकड़ते हैं, शिकारी आये दिन शेर बाघ का शिकार करते हैं उन्हें वे जरा भी डरावने नहीं लगते वरन् उन्हें ढूंढ़ते रहते हैं और मिल जाने पर प्रसन्न होते हैं। जब कि अजनबी व्यक्ति को सांप शेर की तस्वीर देखते और चर्चा सुनने भर से पसीना छूटता है।
अंधेरे में घुसने में डर लगता है। सुनसान में प्रवेश करते हुए पैर कांपते हैं। मन में तरह-तरह की आशंकाएं उठती हैं कि उस अंधेरे—सुनसान में—न जाने क्या विपत्ति होगी। शेर, सांप, बिच्छू, भूत आदि की कितनी आशंकाएं सामने आती हैं और दिल धड़कने लगता है। पर जब उसमें निधड़क प्रवेश किया जाता है—दीपक लेकर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि वहां डरने जैसा कुछ भी नहीं था। मन की दुर्बलता ही है जो जरा-सा आधार मिलते ही तिल का ताड़ बनाती है। काल्पनिक भय गढ़ कर उन्हें इस तरह विचित्र करती है मानो प्राण घाती सर्वनाशी संकट आ गया। अब बचना कठिन है। जबकि वस्तुतः जरा सा कारण ही वहां रहा होता है और वह भी इतना छोटा कि उसके साथ आसानी से निपटा जा सके।
दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अंधेरे में रहते और आते जाते हैं। वन्य प्रदेशों में यदाकदा ही दीपक का प्रयोग होता है। किसान खेतों पर सोते हैं और रात को रखवाली करते हैं। छोटी झोपड़ियां बनाकर सघन जंगलों में लोग परिवारों समेत रहते हैं। धनी लोग सघन बस्ती से हटकर खुले बंगलों में रहते हैं। चोर, डाकू, सांप, बिच्छू, शेर बाघ, भूत पलीत कहां किस को खाते हैं। यदाकदा तो दुर्घटनाएं दिन दहाड़ें बीच बाजार में भी हो सकती हैं। संकट के वास्तविक अवसर कम ही आते हैं। अधिकतर तो लोग काल्पनिक संकट गढ़ते हैं और अपने बनाये उस खिलौने को देख देखकर डरते मरते रहते हैं।
भय वस्तुतः कायरता की प्रतिकृति है। अपना मुंह जैसा भी होगा वैसा ही दर्पण में दीखेगा। आंखों पर पीले कांच का चश्मा पहन लिया जाय तो हर चीज पीली दिखाई देगी। कायर मनुष्य की आन्तरिक दुर्बलता संसार रूपी दर्पण में विपत्ति बनकर दीखती है। संकट का सामना करने की—उससे उलझने, निपटने की क्षमता अपने में नहीं है, यह मान लेने के बाद ही डर आरम्भ होता है। जिसे यह भरोसा है कि कठिन अवसर आवेंगे तो सूझबूझ के साथ उनका मुकाबला करेंगे। उन्हें हटाने के लिए जूझेंगे। इसके लिये अवश्य समझ और बल अपने पास है। मित्र और ईश्वर साथ देगा। इस प्रकार की हिम्मत यदि अपने में मौजूद हो तो काल्पनिक डरों से छुटकारा मिल पाता है और तीन चौथाई मन का बोझ हलका हो जाता है। वास्तविक कारण एक चौथाई होते हैं सो उनके साथ अपने शौर्य को बढ़ाने का व्यायाम समझ कर लड़ा जा सकता है। तैरना, कूदना, मोटर चलाना, व्यायाम प्रतियोगिता, वन पर्वत की यात्रा, यह सभी जोखिम भरे काम हैं। इनमें थोड़ी सी चूक कठिनाई खड़ी कर सकती है पर उस आशंका के कारण कौन उन साहसिक कार्यों का आनन्द छोड़ता है। डर से बचने के उपाय सोचते रहने पर भी उनसे बचे ही रहेंगे इस बात का कोई निश्चय नहीं। बीमारी कौन चाहता है? मौत किसे सुहाती है पर जब आने की घड़ी आ पहुंचती है तो बचने की सारी तरकीबें बेकार चली जाती हैं। निःशंक होकर रहना और जब जो संकट आवेगा उससे निपट लिया जायगा ऐसी हिम्मत रखना, बस संसार में चैन से रहने का यही तरीका है।
भय एक प्रकार की अकड़न है। अकड़न की बीमारी सारे शरीर को जकड़ देती है। अंग सीधे ही नहीं होते, चलना उठना कठिन हो जाता है। रक्त ठण्डा पड़ जाता है और दिमाग सोचना बन्द कर देता है। चाहने पर भी शरीर कुछ काम नहीं करता। लकवा गठिया जैसे रोग ऐसे ही हैं जो जीवित मनुष्य को मृतक जैसा बना देते हैं। उन्हीं में से एक रोग है—भय। डर का अर्थ—पुरुषार्थ की शक्ति रहते हुए भी उसका कुण्ठित हो जाना। सिंह को देखकर हिरन चौकड़ी भरना भूल जाते हैं—खड़े हो जाते हैं और वे मौत मरते हैं। यदि उनमें हिम्मत बनी रहती और छलांग भरते तो प्राणिशास्त्रियों अनुसार हिरन शेर की अपेक्षा अधिक दौड़ को क्या किया जाय। हिम्मत हार जाने पर तो मौत के मुंह में जाने के अलावा और कुछ रास्ता बनता नहीं।
कथा है कि—एक बार यमराज ने महामारी को पृथ्वी पर भेजा और पांच हजार मनुष्य मार लाने के लिए आदेश दिया। बीमारी गई और अपना काम पूरा करके लौट आई। मृतक गिने गये तो वे पन्द्रह हजार थे। यमराज ने डांटा और पूछा—आदेश से तिगुने मृतक क्यों? महामारी ने गम्भीरता पूर्वक कहा—उसने केवल पांच हजार ही मारे हैं। शेष तो डर के मारे खुद ही मर गये हैं।
मानसिक दुर्बलता के अतिरिक्त डर का एक और कारण है—अनैतिकता। जिसकी अन्तरात्मा कलुषित और पाप कर्म से लिप्त है वह कभी चैन की नींद न सो सकेगा। उसे दूसरे की ओर से तरह-तरह की आशंकायें रहेंगी। उन्हें उनसे धोखा होने का—बदला लेने का—फंसा देने का डर बना ही रहेगा। पोल खुल जाने पर बदनामी फैलेगी और लोग सतर्क होकर उसके नाल में फंसने तथा साथ देने से अलग हो जायेंगे। निन्दा और असहयोग की स्थिति में उसका भविष्य ही अन्धकारमय हो जायगा। इस डर से उसका मन सदा आशंकित रहता है। पाप कर्म के फलस्वरूप, समाज का दण्ड, राजदण्ड तथा ईश्वरीय दण्ड मिलते हैं तीनों इकट्ठे होकर या अलग-अलग से वे कभी न कभी मिल कर ही रहेंगे इस भय से भीतर ही भीतर बड़ी बेचैनी रहती है। इस आत्मदेव की पीड़ा उसे निरन्तर टोंचती रहती है। बाहर वाले दण्ड मिलने में तो देर सवेर भी हो सकती है पर आत्म दण्ड तो कुमार्ग पर कदम धरते ही मिलना आरम्भ हो जाता है और वह निरन्तर दुःख देता रहता है।
बेईमान और झूंठा मनुष्य आंखें मिला कर दूसरों को नहीं देख सकता और न जी खोल कर बात करने की हिम्मत पड़ती है। बनावटी उथली उखड़ी बातें करते हुए उसका ओछापन प्रत्यक्ष प्रकट होता रहता है और उसकी मुखाकृति, चेष्टा, भाव-भंगिमा, गतिविधियां वास्तविकता प्रकट करती रहती हैं। अपना आपा ही—चुगली करता है और मूक वाणी से यह घोषित करता रहता है—यहां धोखा ही धोखा है।
कर्जदार अक्सर अनैतिक लोग ही होते हैं। आमदनी से अधिक खर्च करना—चोरी, उठाईगीरी की तरह सर्वथा अनैतिक है। अपनी हैसियत, औकात, आमदनी से बढ़कर ठाट-बाट बनाना, दूसरों को ठगने जैसी कुचेष्टा ही है। ऐसे फिजूलखर्च लोग कर्जदार हो जाते हैं।, चुका पाते नहीं, मित्रों के बीच न उनका विश्वास रह जाता है न सम्मान। जिनका पैसा चाहिये उनसे आंखें चुराते हैं और नये शिकार तलाश करते हैं। ऐसे लोग पग-पग पर डरते हैं कि कर्जदार उनकी इज्जत खराब न कर दें।
सचमुच किसी आकस्मिक मुसीबत में फंस जाने वाला व्यक्ति मित्रों की सहानुभूति का पात्र होता है। वस्तुस्थिति समझ कर लोग उसका सम्मान कम नहीं करते। पर जो फिजूलखर्ची की अनैतिकता अपना कर कर्जदार बना है उसे हर जगह शर्मिन्दगी और लानत का ही सामना करना पड़ेगा। अनैतिकता का हर कदम डराने वाला होता है। चोर और व्यभिचारी बेईमान और अनाचारी व्यक्ति पग-पग पर अपने आस-पास संकट मंडराता देखते हैं। हर किसी को आशंका भरी दृष्टि से देखते हैं कि कहीं किसी को उसके कपट जाल का पता न चल गया हो और कोई उसका भंडाफोड़ न कर दें। यह आशंका अपने आपमें इतनी डरावनी हैं कि मिलने वाले दण्ड की अपेक्षा वह पहले ही मानसिक श्रेष्ठता, स्वभाव और सद्गुणों का नाश कर चुकी होती है।
डर का एक बड़ा कारण अज्ञान भी है। आदिमकाल में मनुष्य को सूर्य ग्रहण, बिजली की कड़क, पुच्छल तारे आदि के बारे में कुछ पता न था। वह इनसे डरता था और देवता समझ कर उनके कोप से बचने के लिये तरह-तरह के पूजन बलिदान करता था। पीछे जब वास्तविकता समझ में आ गई तो वह डर सहज ही चला गया। भूत पलीतों का डर अब धीरे-धीरे समाप्त होता चला जाता है।
ग्रह दशा—जन्म कुण्डली जैसी फलित ज्योतिष की मान्यतायें भी लगभग ऐसी ही हैं। कभी सोचा जाता था कि आसमान में रहने वाले ग्रह नक्षत्र मनुष्यों पर कोप अनुग्रह करते हैं इसी से उसे सुख दुःख मिलते हैं। अब यह प्रकट हो गया है कि यह आकाश में स्थित पिण्ड निर्जीव हैं बहुत दूर हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका किसी को दुख सुख पहुंचा सकना असम्भव है। यह तथ्य समझ में आने पर लोगों ने ग्रह नक्षत्रों से—कल्पित देवी देवताओं से डरना छोड़ दिया है। ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ अनेक प्रकार के डर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।
जिसका भय करना चाहिये उसका नहीं किया जाता और जिनका डर करने की कतई जरूरत नहीं, उनसे डरते रहते हैं। पाप से डरना चाहिए, कर्मफल से डरना चाहिये और ईश्वर के न्याय से। पर इनसे कौन डरता है। चोरी करते हुये, भोले लोगों को ठगते हुए, छल प्रपंच रचते हुये, नशेबाजी, व्यभिचार, बेईमानी, असत्य भाषण करते हुए कौन डरता है? डरते हैं मिट्टी के पुतले मनुष्य से—लोहे के टुकड़ों से बने हथियारों से—काल्पनिक भूत पलीतों से और दीन दुर्बल, कुकर्मी आतंकवादियों से—हमें अपने इस अज्ञान को समझना चाहिये और उस अकिंचन व्यक्तियों वस्तुओं और परिस्थितियों से—डरने से इन्कार कर देना चाहिये जो वस्तुतः तुच्छ एवं असमर्थ हैं। डरना ही हो तो ईश्वर की दण्ड व्यवस्था और दुष्प्रवृत्तियों से डरना चाहिये दुःख तो हमें इन्हीं के कारण मिल सकता है।
इस संसार में भयभीत होने के कोई भी कारण नहीं हैं सिवाय अपने मन की कमजोरी के। यह दुर्बलतायें विचारों और भावनाओं में परिपक्वता के अभाव स्वरूप ही उत्पन्न होती है। यदि विचार, विवेक और समझ-बूझ से काम लिया जाय तो इस प्रकार की दुर्बलताओं का निवारण किया जा सकता है। यद्यपि ये दुर्बलतायें-उत्पन्न होती ही असावधानी वश हैं। फिर भी यदि इन्हें दूर करने के प्रयास किये जायं तो कोई कारण नहीं कि उनका परिमार्जन न किया जा सके।
मस्तिष्क का पूरा नियन्त्रण सारे शरीर पर है, उसकी इच्छा से ही नाड़ी संस्थान काम करता है और ज्ञान तन्तुओं के माध्यम से ही उसी का वर्चस्व छोटे से लेकर बड़े अंगों पर छाया रहता है। ऐसे उद्गम केन्द्र में असन्तुलन पैदा होता हो तो वह स्थानीय नहीं हो सकता, उसका प्रभाव ज्ञान तन्तुओं के माध्यम से अन्य अंगों तक भी पहुंचेगा और वहां भी रुग्णता की संभावना उत्पन्न होगी।
मानसिक घुटन को वाणी द्वारा या क्रिया फूट कर बाहर निकलने का अवसर मिलना चाहिये। अन्यथा वह दबाव अनैच्छिक संस्थान की ओर मुड़ जाता है और शरीर में जो स्वसंचालित क्रियाएं होती रहती हैं उनमें वह घुटन वाला विष जा घुलता है। इससे सम्बन्धित अंगों में सिकुड़न एवं अकड़न पैदा होती है। यदि यह घुटन पेट की ओर मुड़ जाये तो आमाशय पर अकारण ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है और पाचन क्रिया में गड़बड़ मच जाती है। रक्त संचार रुकता है और पाचन रसों की सप्लाई रुक जाती है। उस गड़बड़ी से पहले आमाशय में सूजन होती है फिर जख्म बन जाते हैं। अल्सर इसी प्रकार का रोग है जिसमें शारीरिक कारण कम और मानसिक अधिक रहते हैं।
यदि शोक-सन्ताप का कोई कारण हो तो जोर से रो पड़ने का फूट-फूटकर बिलखने की इच्छा पूरी कर लेनी चाहिये मानसिक आघात से उत्पन्न घुटन बाहर निकाल देने का यही सरल और स्वाभाविक तरीका है। यदि लोक-लाज वश उस इच्छा को दबाकर अपने वीतराग या मनस्वी होने का ढोंग किया जायगा तो मानव स्वभाव की कमजोरियों पर तो विजय पाई न जा सकेगी, वह घुटन भी दबकर भीतर बैठ जायगी और अनेक गड़बड़ियां पैदा करेगी। कोई विषैली चीज पेट में पहुंच जाय तो सीधा तरीका यही है कि उल्टी या दस्त द्वारा बाहर निकल जाने दिया जाय यदि उसे निकलने का अवसर न मिला तो वह विष फिर अनेक भयंकर तरीकों से फूट कर निकलेगा। और दस्त उल्टी जैसी कठिनाई की तुलना में अधिक कष्ट साध्य और समय साध्य होगा।
क्रोध में बकझक कर, जी की जलन शान्त कर लेना अच्छा है। पर यदि उस आवेग को मन में दबा लिया जाय तो वह घृणा या द्वेष के रूप में जड़ जमा कर बैठ जायगा और शत्रुता का रूप धारण करके किसी अवसर पर विकराल प्रतिहिंसा का रूप धारण कर सकता है।
कामुक आकांक्षाओं को होली जैसे त्यौहार पर एक दो दिन उच्छृंखल नाच-कूदकर—गा बजाकर निकाल देते हैं और जी हलका कर लेते हैं इसके विपरीत मन में काम विकार घुमड़ते रहें और बाहर से ब्रह्मचारी बनकर बैठा रहा जाय तो भीतर ही भीतर वह घुटन दूसरे रूप में फूटती है और कई प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न करती है। अच्छा यही है कि मन को ऐसा प्रशिक्षित किया जाय कि उसमें सौम्य सज्जनता ही स्वाभाविक हो जाय और विकार विकृतियों के लिए गुंजाइश ही न रहे। पर यदि क्रोध, शोक आदि आवेग उठ रहे हों तो उन्हें प्रकट होकर बाहर निकल जाने देना चाहिये।
कोई तो ऐसा सच्चा एवं विश्वस्त मित्र होना ही चाहिये जिसके सामने पेट के छिपे हुए हर रहस्य और भेद को प्रकट कर दिया जाय सके। पिछले पापों को भी किसी ऐसे विश्वस्त से कह ही देना चाहिये जो उन्हें हर किसी से कहकर निंदा का वातावरण तो न बनाये पर स्वयं सहानुभूति पूर्वक सुनले। बदले में घृणा भी न करे। छिपी बात को कह सकने योग्य उसे विश्वस्त समझा जाय इसके लिये मित्र की उदारता और आत्मीयता को सराहे। ऐसे मित्रों का होना मनोविकारों की घुटन से पीछा छुड़ाने का अच्छा तरीका है। अपने किये हुए पाप का प्रायश्चित्य कर लेना तो सबसे ही उत्तम है। उससे घुटन द्वारा होने वाली भयंकर संभावनाओं की तुलना में कहीं कम कठिनाई उठाकर, न केवल मन हलका कर लिया जाता है, वरन् कितने ही शारीरिक और मानसिक रोगों की जड़ भी कट जाती हैं।
मनः संस्थान में उत्पन्न घुटन विकृतियां भावनात्मक रोग उत्पन्न करती हैं। उन रोगों के अलग से लक्षण नहीं होते वरन् वे शारीरिक रोगों में मिलकर ही फूटते हैं। शारीरिक रोग यदि काय गत हों तो मामूली दवा-दारू ही अच्छा कर देती है। पुराने समय में जब लोग सरल जीवन जिया करते थे, मन में प्रसन्नता, निष्कपटता और निर्द्वन्दता का सन्तुलन बनाये रहते थे तब आज जैसी मानसिक रोगों की बाढ़ न थी। उस जमाने में केवल काय कष्ट ही होता था अस्तु उनके उपचार में कोई कठिनाई नहीं होती थी। अब प्रत्यक्षतः तो शारीरिक रोग ही दीखते हैं पर उनके पीछे मानसिक रोगों की जटिल ग्रन्थियां उलझी होती हैं, जब तक वे न सुलझें, दवा क्या काम करें। मानसिक रोगों की दवाएं अभी निकली नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि चिकित्सकों को चक्कर में डाल रखने वाले और दवाओं को झुठलाते रहने वाले रोगों का बाहुल्य औषधि उपचार की परिधि से बाहर निकलने लगे तो उसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं है।
भावनाएं यदि निर्मल उदात्त और उच्चस्तरीय हों तो उनसे हर दृष्टि में लाभ ही लाभ है। अन्तःकरण मस्तिष्क और शरीर इन तीनों की ही पुष्टि होती है। परिस्थिति वश यदि शोक, क्रोध जैसे अवसर आ जायं और विवेक उनके समाधान में समर्थ न हो तो उसे स्वाभाविक रीति से प्रकट हो जाने देना चाहिए। जितना सम्भव हो उतना मर्यादाओं का पालन किया जाय, विवेक द्वारा बड़ी दीखने वाली बात को छोटी करके उपेक्षा में डाल दिया जाय पर यदि वैसा न बन पड़े तो उसके प्रकटीकरण में भी हर्ज नहीं है।
कामवासना के पीछे मूलवृत्ति हास्य, विनोद और क्रीड़ा कल्लोल की—कोमल भावनाओं की उत्तेजना का आनन्द लेने की होती है। उसे दूसरे रूप में प्रकट और परिणत किया जा सकता है। छोटे बालकों को खिलाने, दुलारने से भी सौन्दर्य वासना और निर्मल हास, विलास की आवश्यकता पूरी हो जाती है। संगीत साहित्य जैसी ललित कलाओं का निर्माण ही इस आधार पर हुआ है कि उनसे भावनात्मक नीरसता को सरसता में परिणत होने का अवसर मिले। नर-नारी में भी निष्पाप हास्य विनोद चलता रह सकता है। कुटुम्ब में बहिन, भाई, देवर, भौजाई, चाची, भतीजे जैसे कई रिश्ते नर-नारी के बीच रहते हैं। इनमें परस्पर विचार विनिमय, हास्य-परिहास, वार्तालाप चलता रहे तो नर-नारी की पूरक आकांक्षाएं पवित्र स्तर पर पूरी होती रह सकती हैं और कामेच्छा का उदात्तीकरण होने से उन्हें भावनात्मक तृप्ति मिलती रह सकती है। पति-पत्नी के बीच भी शरीरों को न्यूनतम मात्रा में ही गला कर—व्यंग विनोद, उपहास-परिहास की शालीन प्रक्रिया अपनाकर मनःक्षेत्र को उल्लास भरा जा सकता है और वासना जन्य घुटन का सहज निष्कासन होता रह सकता है। इस स्थिति में ब्रह्मचर्य पालन कठिन नहीं पड़ता वरन् सरल हो जाता है।
भावनाओं का अनियन्त्रित उभार ठीक शरीर में चढ़े हुए बुखार की तरह है। बुखार में पाचन तन्त्र लड़खड़ा जाता है। कोई अवयव उत्तेजित होकर, अधिक काम कर रहा होता है कोई एकदम शिथिल पड़ गया होता है। ऐसे असन्तुलन में रोगी को दाह, प्यास, बेचैनी, दर्द आदि कितने ही कष्ट अनुभव होते हैं। भावनात्मक उभार को एक मस्तिष्कीय बुखार कहना चाहिये। कई बार वह तीव्र होता है कई बार मन्द। क्रोध, शोक और बेकाबू होकर प्रकट होने वाले आवेग तीव्र बुखार है। चिन्ता, निराशा, कुढ़न, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियां मन्द ज्वर हैं। आकांक्षाओं को इतनी बढ़ा लेना कि वर्तमान परिस्थिति में कार्यान्वित फलीभूत न हो सकें तो भी उनसे अतृप्ति जन्य क्षोभ उत्पन्न होता है और मानसिक सन्तुलन बिगड़ता है। उन्नति के लिए प्रयत्न करना बात अलग है। और महत्वाकांक्षाओं का पहाड़ खड़ा करके हर घड़ी असन्तोष का अनुभव करना बिलकुल अलग बात है। कितने ही व्यक्ति उपलब्धियों के लिए व्यवस्थित प्रयास तो कम करते हैं, कामनाओं के रंग-बिरंगे स्वप्न देखते रहते हैं। शेखचिल्ली की तरह लम्बी-चौड़ी बातें सोचते रहना तो सरल है पर उन्हें फलीभूत बनाने के लिये योग्यता साधन और परिस्थिति तीनों का ही तालमेल रहना चाहिये। इसके बिना महत्वाकांक्षाएं—ऐषणाएं केवल मानसिक विक्षोभ ही दे सकती हैं इस प्रकार की उड़ानें उड़ते रहने वाले अन्ततः निराशा जन्य मानसिक रोगों के जाल जंजाल में जा फंसते हैं।
भावनात्मक विकृतियां शरीर के उपयोगी अंगों पर तथा जीवन संचार की क्रियाओं पर बुरा असर डालती हैं उनके सामान्य क्रम को लड़खड़ा देती हैं और वह अवरोध किसी न किसी शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होता है। पापी मनुष्य दूसरों की जितनी हानि करता है। उससे ज्यादा अपनी करता है। दुष्कर्म कर लेना अपने हाथ की बात है पर उसकी प्रतिक्रिया जो कर्त्ता के ऊपर होती है, और आत्म धिक्कार की आत्म-प्रताड़ना की, जो भीतर ही भीतर मार पड़ती है उसे रोकना किसी के वश में नहीं रहता। पाप पुण्य के भले-बुरे फल मिलने की यही तो स्वसंचालित प्रक्रिया है। पाप कर्म के बाद अन्तःकरण में अनायास ही पश्चाताप और धिक्कार की प्रतिक्रिया उठती है। उससे शरीर और मन का सन्तुलन बिगड़ता है। दोनों क्षेत्र रुग्ण होते हैं। उसके फलस्वरूप जन-सहयोग का अभाव, असम्मान मिलता है। और सन्तुलन बिगड़ा रहने से हाथ में लिये हुए काम असफल होते हैं। इस सबका मिला-जुला स्वरूप शारीरिक मानसिक कष्ट के रूप में आधि-व्याधि बनकर सामने आता है। कर्मफल भोग की यही मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इससे बचाव करने के लिये निष्पाप जीवन क्रम अपनाने की आवश्यकता है। जो पाप पिछले दिन बन पड़े हैं उनके प्रायश्चित के लिये किसी सूक्ष्मदर्शी आत्मविद्या विज्ञानी से परामर्श लेने की आवश्यकता है।
‘साइको सोमेटिक’ रोगों की बाढ़ इन दिनों बौद्धिक विकास के दुरुपयोग ने उत्पन्न की है। होना यह चाहिए कि यदि प्रबुद्धता के दुरुपयोग का खतरा हो वहां मानसिक विकास का प्रयास न किया जाय यदि वह अनुचित लगता है और मस्तिष्कीय विकास आवश्यक लगता है तो उसे सन्मार्गगामी बनाये जाने की समुचित तैयारी पहले से ही रखनी चाहिये। विकसित मस्तिष्क यदि दुष्प्रवृत्तियों से भरा रहा तो निश्चित रूप ले वह अभिशाप सिद्ध होगा और उसका दंड जटिल कष्ट साध्य, दुराग्रही साइकोसोमेटिक रोगों के रूप में भुगतना पड़ेगा। यह मानसिक रोग झक्कापन, सनक, आवेश, मतिभ्रम, अर्ध विक्षिप्तावस्था, पागलपन आदि के रूप में भी हो सकते हैं और अन्य शारीरिक अवयवों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं।
घुटन एक—न दीखने वाली—न समझ में आने वाली बीमारी है, पर इसका कुप्रभाव किसी भी भयंकर रोग से कम नहीं होता। अतृप्त और असंतुष्ट मनुष्य अपने आप ही अपने आप को खाता, खोता और खोखला करता रहता है। घुटन से बचा जाय। यदि अपनी भूल है—स्थिति का सही मूल्यांकन न करके काल्पनिक जाल-जंजाल बुन लिया गया है तो मकड़ी के जाले को तोड़कर यथार्थता के धरातल पर आना चाहिये और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर मन का बोझ हलका करना चाहिये। यदि अपनी मान्यता सही है और दबाव डालकर आत्मा की आवाज का हनन किया जा रहा है तो फिर ऐसे आधिपत्य से इनकार करके अपना स्वतन्त्र रास्ता बनाना चाहिये फिर चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। घुटन में दिन काटते हुए अन्तरात्मा को दिन-दिन दुर्बल बनाते जाने से तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही बल नष्ट होते हैं। इस प्रकार आत्महत्या की स्थिति से तो निकलना ही चाहिए भले ही उसमें कुछ बड़ा जोखिम उठाना पड़े। घुटन यदि आत्म प्रताड़ना की है तो उसे किसी विश्वस्त मित्र के आगे जी खोलकर कह ही देना चाहिये इस प्रकार वह धुंआ बाहर निकाल देने पर ही जी हलका हो सकता है।
उसी से डरें जिससे डरना चाहिए—
संकट भयंकर जब तक लगता है जब तक उसके साथ मुठभेड़ नहीं होती। जब उसके साथ गुंथ जाया जाता है और मानसिक सन्तुलन बिगड़ने नहीं दिया जाता तो प्रतीत होता है कि जितना सोचा गया था—उससे आधी चौथाई भी उसकी वास्तविक भयानकता नहीं थी। संकटों के साथ गुंथने का जैसे-जैसे अभ्यास होता जाता है, वैसे-वैसे वे स्वाभाविक दैनिक कार्यों की तरह सरल प्रतीत होने लगते हैं।
अपने लिये सांप और शेर बहुत भयंकर होते हैं पर बहुत से लोगों का धन्धा ही उन्हें पकड़ना मारना है। सपेरे रोज ही काले विषधर नाग पकड़ते हैं, शिकारी आये दिन शेर बाघ का शिकार करते हैं उन्हें वे जरा भी डरावने नहीं लगते वरन् उन्हें ढूंढ़ते रहते हैं और मिल जाने पर प्रसन्न होते हैं। जब कि अजनबी व्यक्ति को सांप शेर की तस्वीर देखते और चर्चा सुनने भर से पसीना छूटता है।
अंधेरे में घुसने में डर लगता है। सुनसान में प्रवेश करते हुए पैर कांपते हैं। मन में तरह-तरह की आशंकाएं उठती हैं कि उस अंधेरे—सुनसान में—न जाने क्या विपत्ति होगी। शेर, सांप, बिच्छू, भूत आदि की कितनी आशंकाएं सामने आती हैं और दिल धड़कने लगता है। पर जब उसमें निधड़क प्रवेश किया जाता है—दीपक लेकर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि वहां डरने जैसा कुछ भी नहीं था। मन की दुर्बलता ही है जो जरा-सा आधार मिलते ही तिल का ताड़ बनाती है। काल्पनिक भय गढ़ कर उन्हें इस तरह विचित्र करती है मानो प्राण घाती सर्वनाशी संकट आ गया। अब बचना कठिन है। जबकि वस्तुतः जरा सा कारण ही वहां रहा होता है और वह भी इतना छोटा कि उसके साथ आसानी से निपटा जा सके।
दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अंधेरे में रहते और आते जाते हैं। वन्य प्रदेशों में यदाकदा ही दीपक का प्रयोग होता है। किसान खेतों पर सोते हैं और रात को रखवाली करते हैं। छोटी झोपड़ियां बनाकर सघन जंगलों में लोग परिवारों समेत रहते हैं। धनी लोग सघन बस्ती से हटकर खुले बंगलों में रहते हैं। चोर, डाकू, सांप, बिच्छू, शेर बाघ, भूत पलीत कहां किस को खाते हैं। यदाकदा तो दुर्घटनाएं दिन दहाड़ें बीच बाजार में भी हो सकती हैं। संकट के वास्तविक अवसर कम ही आते हैं। अधिकतर तो लोग काल्पनिक संकट गढ़ते हैं और अपने बनाये उस खिलौने को देख देखकर डरते मरते रहते हैं।
भय वस्तुतः कायरता की प्रतिकृति है। अपना मुंह जैसा भी होगा वैसा ही दर्पण में दीखेगा। आंखों पर पीले कांच का चश्मा पहन लिया जाय तो हर चीज पीली दिखाई देगी। कायर मनुष्य की आन्तरिक दुर्बलता संसार रूपी दर्पण में विपत्ति बनकर दीखती है। संकट का सामना करने की—उससे उलझने, निपटने की क्षमता अपने में नहीं है, यह मान लेने के बाद ही डर आरम्भ होता है। जिसे यह भरोसा है कि कठिन अवसर आवेंगे तो सूझबूझ के साथ उनका मुकाबला करेंगे। उन्हें हटाने के लिए जूझेंगे। इसके लिये अवश्य समझ और बल अपने पास है। मित्र और ईश्वर साथ देगा। इस प्रकार की हिम्मत यदि अपने में मौजूद हो तो काल्पनिक डरों से छुटकारा मिल पाता है और तीन चौथाई मन का बोझ हलका हो जाता है। वास्तविक कारण एक चौथाई होते हैं सो उनके साथ अपने शौर्य को बढ़ाने का व्यायाम समझ कर लड़ा जा सकता है। तैरना, कूदना, मोटर चलाना, व्यायाम प्रतियोगिता, वन पर्वत की यात्रा, यह सभी जोखिम भरे काम हैं। इनमें थोड़ी सी चूक कठिनाई खड़ी कर सकती है पर उस आशंका के कारण कौन उन साहसिक कार्यों का आनन्द छोड़ता है। डर से बचने के उपाय सोचते रहने पर भी उनसे बचे ही रहेंगे इस बात का कोई निश्चय नहीं। बीमारी कौन चाहता है? मौत किसे सुहाती है पर जब आने की घड़ी आ पहुंचती है तो बचने की सारी तरकीबें बेकार चली जाती हैं। निःशंक होकर रहना और जब जो संकट आवेगा उससे निपट लिया जायगा ऐसी हिम्मत रखना, बस संसार में चैन से रहने का यही तरीका है।
भय एक प्रकार की अकड़न है। अकड़न की बीमारी सारे शरीर को जकड़ देती है। अंग सीधे ही नहीं होते, चलना उठना कठिन हो जाता है। रक्त ठण्डा पड़ जाता है और दिमाग सोचना बन्द कर देता है। चाहने पर भी शरीर कुछ काम नहीं करता। लकवा गठिया जैसे रोग ऐसे ही हैं जो जीवित मनुष्य को मृतक जैसा बना देते हैं। उन्हीं में से एक रोग है—भय। डर का अर्थ—पुरुषार्थ की शक्ति रहते हुए भी उसका कुण्ठित हो जाना। सिंह को देखकर हिरन चौकड़ी भरना भूल जाते हैं—खड़े हो जाते हैं और वे मौत मरते हैं। यदि उनमें हिम्मत बनी रहती और छलांग भरते तो प्राणिशास्त्रियों अनुसार हिरन शेर की अपेक्षा अधिक दौड़ को क्या किया जाय। हिम्मत हार जाने पर तो मौत के मुंह में जाने के अलावा और कुछ रास्ता बनता नहीं।
कथा है कि—एक बार यमराज ने महामारी को पृथ्वी पर भेजा और पांच हजार मनुष्य मार लाने के लिए आदेश दिया। बीमारी गई और अपना काम पूरा करके लौट आई। मृतक गिने गये तो वे पन्द्रह हजार थे। यमराज ने डांटा और पूछा—आदेश से तिगुने मृतक क्यों? महामारी ने गम्भीरता पूर्वक कहा—उसने केवल पांच हजार ही मारे हैं। शेष तो डर के मारे खुद ही मर गये हैं।
मानसिक दुर्बलता के अतिरिक्त डर का एक और कारण है—अनैतिकता। जिसकी अन्तरात्मा कलुषित और पाप कर्म से लिप्त है वह कभी चैन की नींद न सो सकेगा। उसे दूसरे की ओर से तरह-तरह की आशंकायें रहेंगी। उन्हें उनसे धोखा होने का—बदला लेने का—फंसा देने का डर बना ही रहेगा। पोल खुल जाने पर बदनामी फैलेगी और लोग सतर्क होकर उसके नाल में फंसने तथा साथ देने से अलग हो जायेंगे। निन्दा और असहयोग की स्थिति में उसका भविष्य ही अन्धकारमय हो जायगा। इस डर से उसका मन सदा आशंकित रहता है। पाप कर्म के फलस्वरूप, समाज का दण्ड, राजदण्ड तथा ईश्वरीय दण्ड मिलते हैं तीनों इकट्ठे होकर या अलग-अलग से वे कभी न कभी मिल कर ही रहेंगे इस भय से भीतर ही भीतर बड़ी बेचैनी रहती है। इस आत्मदेव की पीड़ा उसे निरन्तर टोंचती रहती है। बाहर वाले दण्ड मिलने में तो देर सवेर भी हो सकती है पर आत्म दण्ड तो कुमार्ग पर कदम धरते ही मिलना आरम्भ हो जाता है और वह निरन्तर दुःख देता रहता है।
बेईमान और झूंठा मनुष्य आंखें मिला कर दूसरों को नहीं देख सकता और न जी खोल कर बात करने की हिम्मत पड़ती है। बनावटी उथली उखड़ी बातें करते हुए उसका ओछापन प्रत्यक्ष प्रकट होता रहता है और उसकी मुखाकृति, चेष्टा, भाव-भंगिमा, गतिविधियां वास्तविकता प्रकट करती रहती हैं। अपना आपा ही—चुगली करता है और मूक वाणी से यह घोषित करता रहता है—यहां धोखा ही धोखा है।
कर्जदार अक्सर अनैतिक लोग ही होते हैं। आमदनी से अधिक खर्च करना—चोरी, उठाईगीरी की तरह सर्वथा अनैतिक है। अपनी हैसियत, औकात, आमदनी से बढ़कर ठाट-बाट बनाना, दूसरों को ठगने जैसी कुचेष्टा ही है। ऐसे फिजूलखर्च लोग कर्जदार हो जाते हैं।, चुका पाते नहीं, मित्रों के बीच न उनका विश्वास रह जाता है न सम्मान। जिनका पैसा चाहिये उनसे आंखें चुराते हैं और नये शिकार तलाश करते हैं। ऐसे लोग पग-पग पर डरते हैं कि कर्जदार उनकी इज्जत खराब न कर दें।
सचमुच किसी आकस्मिक मुसीबत में फंस जाने वाला व्यक्ति मित्रों की सहानुभूति का पात्र होता है। वस्तुस्थिति समझ कर लोग उसका सम्मान कम नहीं करते। पर जो फिजूलखर्ची की अनैतिकता अपना कर कर्जदार बना है उसे हर जगह शर्मिन्दगी और लानत का ही सामना करना पड़ेगा। अनैतिकता का हर कदम डराने वाला होता है। चोर और व्यभिचारी बेईमान और अनाचारी व्यक्ति पग-पग पर अपने आस-पास संकट मंडराता देखते हैं। हर किसी को आशंका भरी दृष्टि से देखते हैं कि कहीं किसी को उसके कपट जाल का पता न चल गया हो और कोई उसका भंडाफोड़ न कर दें। यह आशंका अपने आपमें इतनी डरावनी हैं कि मिलने वाले दण्ड की अपेक्षा वह पहले ही मानसिक श्रेष्ठता, स्वभाव और सद्गुणों का नाश कर चुकी होती है।
डर का एक बड़ा कारण अज्ञान भी है। आदिमकाल में मनुष्य को सूर्य ग्रहण, बिजली की कड़क, पुच्छल तारे आदि के बारे में कुछ पता न था। वह इनसे डरता था और देवता समझ कर उनके कोप से बचने के लिये तरह-तरह के पूजन बलिदान करता था। पीछे जब वास्तविकता समझ में आ गई तो वह डर सहज ही चला गया। भूत पलीतों का डर अब धीरे-धीरे समाप्त होता चला जाता है।
ग्रह दशा—जन्म कुण्डली जैसी फलित ज्योतिष की मान्यतायें भी लगभग ऐसी ही हैं। कभी सोचा जाता था कि आसमान में रहने वाले ग्रह नक्षत्र मनुष्यों पर कोप अनुग्रह करते हैं इसी से उसे सुख दुःख मिलते हैं। अब यह प्रकट हो गया है कि यह आकाश में स्थित पिण्ड निर्जीव हैं बहुत दूर हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका किसी को दुख सुख पहुंचा सकना असम्भव है। यह तथ्य समझ में आने पर लोगों ने ग्रह नक्षत्रों से—कल्पित देवी देवताओं से डरना छोड़ दिया है। ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ अनेक प्रकार के डर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।
जिसका भय करना चाहिये उसका नहीं किया जाता और जिनका डर करने की कतई जरूरत नहीं, उनसे डरते रहते हैं। पाप से डरना चाहिए, कर्मफल से डरना चाहिये और ईश्वर के न्याय से। पर इनसे कौन डरता है। चोरी करते हुये, भोले लोगों को ठगते हुए, छल प्रपंच रचते हुये, नशेबाजी, व्यभिचार, बेईमानी, असत्य भाषण करते हुए कौन डरता है? डरते हैं मिट्टी के पुतले मनुष्य से—लोहे के टुकड़ों से बने हथियारों से—काल्पनिक भूत पलीतों से और दीन दुर्बल, कुकर्मी आतंकवादियों से—हमें अपने इस अज्ञान को समझना चाहिये और उस अकिंचन व्यक्तियों वस्तुओं और परिस्थितियों से—डरने से इन्कार कर देना चाहिये जो वस्तुतः तुच्छ एवं असमर्थ हैं। डरना ही हो तो ईश्वर की दण्ड व्यवस्था और दुष्प्रवृत्तियों से डरना चाहिये दुःख तो हमें इन्हीं के कारण मिल सकता है।
इस संसार में भयभीत होने के कोई भी कारण नहीं हैं सिवाय अपने मन की कमजोरी के। यह दुर्बलतायें विचारों और भावनाओं में परिपक्वता के अभाव स्वरूप ही उत्पन्न होती है। यदि विचार, विवेक और समझ-बूझ से काम लिया जाय तो इस प्रकार की दुर्बलताओं का निवारण किया जा सकता है। यद्यपि ये दुर्बलतायें-उत्पन्न होती ही असावधानी वश हैं। फिर भी यदि इन्हें दूर करने के प्रयास किये जायं तो कोई कारण नहीं कि उनका परिमार्जन न किया जा सके।